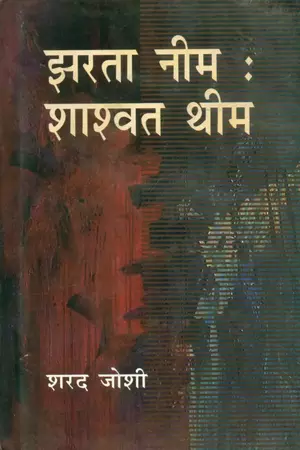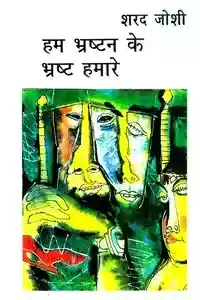|
हास्य-व्यंग्य >> झरता नीम : शाश्वत थीम झरता नीम : शाश्वत थीमशरद जोशी
|
356 पाठक हैं |
|||||||
"शरद जोशी का साहित्य : सरलता में छिपी असाधारणता और मानवीय दृष्टि की गहरी पहचान।"
Jharta Neem Shashvat Theem
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
लोग जितना समझते हैं, शरद जोशी का साहित्य उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अपने जीवन काल में वे लिखने में जितना व्यस्त रहे, उतना ही अपनी कृतियों को पुस्तक रूप में छापने में उदासीन रहे। वैसे, उनके जीवन काल में उनकी कई कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थीं। शरद जोशी का लेखन ऊपर से देखने पर निहायत सीधा-सादा और साधारण लगता है पर दुबारा पढ़ते ही अपनी असाधारणता से पाठक को अभिभूत कर देता है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो यह की साधारण स्थिति पर हल्के फुलके ढंग से लिखते हुए वे अचानक किसी अप्रत्याशित कोण से हमारी चेतना पर हमला करते हैं। अप्रत्याशित-शरद जोशी के लेखन में कहीं भी मिल सकते हैं।
उनकी दूसरी खूबी उनके अत्यन्त मनोहर, मानवीय स्वभाव में है जो उनकी रचनाओं में सर्वत्र प्रतिफलित है। हास्य और व्यंग्य की शास्त्रीय विश्लेषण करनेवाले व्यंग्य को सामाजिक जीवन की तीखी आलोचना से जोड़ते हैं। जहाँ विरूपता, बिडम्बना, अतिश्योक्ति, फूहड़पन और जुगुप्सा आदि कुछ भी वर्जित नहीं है। शरद जोशी व्यंग्य और हास्य की इस चिरन्तन और शास्त्रीय अन्तर को अपने सहज सौम्य स्वभाव से मिटाते नजर आते हैं। वे समाज के विविध पक्षों की तीखी आलोचना करते हुए भी अपने तीखेपन को छिपाये बिना भी कटुता और अमर्यादित भर्त्सना से उसे दूर रखते हैं।
शरद जोशी के लेखन में पाठक देखेंगे कि उनमें अधिकांशतः वाचिक परम्परा की रचनाएँ हैं। ऐसा लगा रहा है कि लेखक नहीं लिख रहा है, वह एक अंतरंग समुदाय से बात कर रहा है और यह तब की बात है जब शरद जोशी सार्वजनिक रूप के श्रोताओं के आगे अपनी रचनाएँ नहीं पढ़ते थे, उन्हें केवल एकान्त में लिखते थे।
मुझे विश्वास है कि शरद जोशी का यह संग्रह उनकी कीर्ति को और भी परिपुष्ट करेगा, उनके यशःकाय की उपस्थिति को हमारे बीच और भी जीवन्त बनायेगा।
एक जमाना था, जब यह पंक्ति मशहूर थी कि ‘जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।’ अँग्रेजों के पास तोपें थीं और उसके मुकाबले में भारतवासी अखबारों का प्रकाशन करते थे। ‘हरिजन’ छापना गाँधी जी के लिए एक अहिंसक क्रिया थी। अत्याचारों के विरुद्ध विचारों की लड़ाई। उन दिनों सभी हिन्दी पत्र राष्ट्रीय और अखिल भारतीय होते थे। उन दिनों छपे अखबारों को घूम-घूमकर बेचना देश और समाज की सेवा मानी जाती थी। आज जो काँग्रेसी मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, इनके बाप और चाचा यह काम बड़े उत्साह और लगन से करते थे। अँग्रेजों के पास तोपें थी, काँग्रेसियों के पास अखबार। इन राजनेताओं के चरित्र में जो आदर्शवादिता का अंश राजनीतिक कैरियर के आरंभिक वर्षों में नजर आता था, वह ऐसे ही अखबारों का प्रभाव था। इन होनहार बिरवानों के पत्तों पर जो आशा जगानेवाला चिकनापन शुरु में था, वह बड़ी हद तक अखबारों को देना था। समाज में इनकी आरंभिक तुतलाहट अखबार की भाषा बोलने के कारण दूर हुई इनके अधकच्चे, अधकचरे सार्वजनिक प्रलापों को अखबारों ने आकार-प्रकार और सुधार देकर प्रकाशित किया, जिससे इनके ऊबड़-खाबड़ व्यक्तित्व को सँवरने का मौका मिला।
उनकी दूसरी खूबी उनके अत्यन्त मनोहर, मानवीय स्वभाव में है जो उनकी रचनाओं में सर्वत्र प्रतिफलित है। हास्य और व्यंग्य की शास्त्रीय विश्लेषण करनेवाले व्यंग्य को सामाजिक जीवन की तीखी आलोचना से जोड़ते हैं। जहाँ विरूपता, बिडम्बना, अतिश्योक्ति, फूहड़पन और जुगुप्सा आदि कुछ भी वर्जित नहीं है। शरद जोशी व्यंग्य और हास्य की इस चिरन्तन और शास्त्रीय अन्तर को अपने सहज सौम्य स्वभाव से मिटाते नजर आते हैं। वे समाज के विविध पक्षों की तीखी आलोचना करते हुए भी अपने तीखेपन को छिपाये बिना भी कटुता और अमर्यादित भर्त्सना से उसे दूर रखते हैं।
शरद जोशी के लेखन में पाठक देखेंगे कि उनमें अधिकांशतः वाचिक परम्परा की रचनाएँ हैं। ऐसा लगा रहा है कि लेखक नहीं लिख रहा है, वह एक अंतरंग समुदाय से बात कर रहा है और यह तब की बात है जब शरद जोशी सार्वजनिक रूप के श्रोताओं के आगे अपनी रचनाएँ नहीं पढ़ते थे, उन्हें केवल एकान्त में लिखते थे।
मुझे विश्वास है कि शरद जोशी का यह संग्रह उनकी कीर्ति को और भी परिपुष्ट करेगा, उनके यशःकाय की उपस्थिति को हमारे बीच और भी जीवन्त बनायेगा।
एक जमाना था, जब यह पंक्ति मशहूर थी कि ‘जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।’ अँग्रेजों के पास तोपें थीं और उसके मुकाबले में भारतवासी अखबारों का प्रकाशन करते थे। ‘हरिजन’ छापना गाँधी जी के लिए एक अहिंसक क्रिया थी। अत्याचारों के विरुद्ध विचारों की लड़ाई। उन दिनों सभी हिन्दी पत्र राष्ट्रीय और अखिल भारतीय होते थे। उन दिनों छपे अखबारों को घूम-घूमकर बेचना देश और समाज की सेवा मानी जाती थी। आज जो काँग्रेसी मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, इनके बाप और चाचा यह काम बड़े उत्साह और लगन से करते थे। अँग्रेजों के पास तोपें थी, काँग्रेसियों के पास अखबार। इन राजनेताओं के चरित्र में जो आदर्शवादिता का अंश राजनीतिक कैरियर के आरंभिक वर्षों में नजर आता था, वह ऐसे ही अखबारों का प्रभाव था। इन होनहार बिरवानों के पत्तों पर जो आशा जगानेवाला चिकनापन शुरु में था, वह बड़ी हद तक अखबारों को देना था। समाज में इनकी आरंभिक तुतलाहट अखबार की भाषा बोलने के कारण दूर हुई इनके अधकच्चे, अधकचरे सार्वजनिक प्रलापों को अखबारों ने आकार-प्रकार और सुधार देकर प्रकाशित किया, जिससे इनके ऊबड़-खाबड़ व्यक्तित्व को सँवरने का मौका मिला।
काहे की आत्मा और कैसा कथ्य ?
हिन्दी में लेखक होने का अर्थ है, निरंतर उन निगाहों द्वारा घूरे जाना, जो आपको अपराधी समझती हैं। साहित्य में या महज जीवन जीने के लिए आप कुछ कीजिए, वे निगाहें आपको लगातार यह एहसास देंगी कि आप गलत हैं, घोर स्वार्थी हैं, हलके हैं आदि। लेखक के रूप में आप यात्री बनें, तो यह तैयारी आप मन में कर लेते हैं कि यात्रा कठिन होगी, मंजिल अनिश्चित और अनजानी है, सुख केवल चलने और चलते रहने भर का है। पर शीघ्र ही आपको पता लगता है कि कोई आपका खेदा कर रहा है और कुछ लोग आपका सामना करने के लिए खड़े हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मलतब, आप जैसे चलना चाहते हैं, वैसे चल क्यों नहीं सकते ? जो पीछे से खेदा कर रहा है, वह आपकी पीठ पर वार क्यों करना चाहता है और जो सामने खड़े हमलावर आपके रास्ते में बाधक हैं, उनकी आपसे नाराजगी क्या है ?
आप चाहते हैं कि कन्नी काटकर निकल जाएँ, मगर लिखने के इस रास्ते पर जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रास्ता बजाय प्रशस्त होने के, सँकरा होता जाता है। कन्नी काट नहीं सकते। सँकरे रास्ते और तंगदिल लोगों के आक्रामक समूहों से जूझते हुए चलने का प्रयत्न करना, साहित्य में जीना है।
आप चाहते हैं कि कन्नी काटकर निकल जाएँ, मगर लिखने के इस रास्ते पर जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रास्ता बजाय प्रशस्त होने के, सँकरा होता जाता है। कन्नी काट नहीं सकते। सँकरे रास्ते और तंगदिल लोगों के आक्रामक समूहों से जूझते हुए चलने का प्रयत्न करना, साहित्य में जीना है।
मध्यमार्ग से क्यों चला जाए ?
ऐसे में लेखक की तरह जी लेने की केवल दो ही स्थितियाँ संभव हैं। एक यह कि आप अपराधबोध से ग्रस्त रहें और धीरे-धीरे मुरझा जाएँ। मतलब, आप नाम भर के लेखक रहें और शेष यात्रा घिसटते, घिघियाते तय करें। दूसरी यह कि आप एक किस्म की बेशर्मी अख्तियार कर लें, लापरवाह हो जाएँ। यों कि आप आपने को हाथी समझ लें और भौंकने-गुर्रानेवालों की बिना चिन्ता किए, बाजार से गुजर जाएँ। पहली स्थिति में आप लेखक ही नहीं रहते, उन अर्थों में, जिनमें लेखक परिभाषित होता है। दूसरी स्थिति में आप उन सारे रिश्तों को तोड़ देते हैं, जो जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं, होने चाहिए।
इस समय हिन्दी के सारे लेखक और लेखक कहलाने वाले, इन दोनों में से किसी एक स्थिति में जी रहे हैं। मैं दूसरी बेशर्म-सी हालत में जी रहा हूँ। अपनी सफाई में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं इस तरह जीना कभी नहीं चाहता था। मैं बड़ों के प्रति अत्यधिक आदर, बराबरी के लेखकों से खुली दोस्ती और अपने से छोटे लेखकों को पर्याप्त स्नेह देते हुए, हिन्दी लेखन की इस दुनिया में कुछ जिम्मेदारियाँ निभाते हुए, अपनी उम्र काट लेना चाहता था। पर इस हिन्दी में लेखक का आसपास बहुत भयानक और निर्मम होता है। वह हमला न भी करे, उसे बचाव की लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। यह कहना बहुत पीड़ादायक है कि मैं बहुत धीरे-धीरे और बहुत मजबूरी से, पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में आया। किस्तों में, धकियाया जाकर।
मैं सफाई दे रहा हूँ, पर हिन्दी लेखन में अपनी सफाई जैसी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ केवल आरोप लगते हैं और निर्णय दिए जाते हैं। बल्कि आरोप ही अन्तिम निर्णय होते हैं। यह विचित्र अदालत है, जहाँ आपसे केवल सजा भुगतने की अपेक्षा की जाती है। ‘आत्मकथा’ एक शब्द भर है। यहाँ आत्मा को शक से देखा जाता है और कथ्य पर कोई भरोसा नहीं करता। जिस दिन कोई कह दे कि आप अपराधी हैं, बस उस दिन से आप अपराधी हैं।
लगातार सजा भुगतने की इस लेखकवाली जिंदगी में आप प्रायः जानना चाहते हैं कि आपका अपराध क्या है ? यह कोई नहीं बताएगा कि क्या विधान है, जिसका उल्लंघन करना दोष है। आपको पता लगेगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं, वही आपका अपराध है। हिन्दी में लेखक होने का अर्थ है, निरंतर कठघरे में खड़े रहना और वकीलों और न्यायधीशों की एक अनचाही, बिनबुलाई और प्रायः बदलती भीड़ द्वारा फतवे सुनना। आपकी यही नियति है। यह सब देख कर आपकी सिर पीटने की इच्छा होती है। उत्तेजित आप रहते हैं। अक्सर हिन्दी का ईमानदार लेखक भ्रम और उत्तेजना के बीच की जिंन्दगी जीता है। निराला सृजन के मामले में निराले थे, पर वे उदाहरण इसी तथ्य के हैं। जो तनिक भी निराले नहीं हैं, उदाहरण वे भी इसी परम तथ्य के हैं। अपना सिर पीटिए और यह जानने का प्रयत्न कीजिए कि लोग आपका सिर क्यों तोड़ने पर तुले हैं ? हिन्दी में लिखने का अर्थ निरंतर प्रहारों से सिर बचाना है, बेशर्मी से।
इस समय हिन्दी के सारे लेखक और लेखक कहलाने वाले, इन दोनों में से किसी एक स्थिति में जी रहे हैं। मैं दूसरी बेशर्म-सी हालत में जी रहा हूँ। अपनी सफाई में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं इस तरह जीना कभी नहीं चाहता था। मैं बड़ों के प्रति अत्यधिक आदर, बराबरी के लेखकों से खुली दोस्ती और अपने से छोटे लेखकों को पर्याप्त स्नेह देते हुए, हिन्दी लेखन की इस दुनिया में कुछ जिम्मेदारियाँ निभाते हुए, अपनी उम्र काट लेना चाहता था। पर इस हिन्दी में लेखक का आसपास बहुत भयानक और निर्मम होता है। वह हमला न भी करे, उसे बचाव की लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। यह कहना बहुत पीड़ादायक है कि मैं बहुत धीरे-धीरे और बहुत मजबूरी से, पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में आया। किस्तों में, धकियाया जाकर।
मैं सफाई दे रहा हूँ, पर हिन्दी लेखन में अपनी सफाई जैसी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ केवल आरोप लगते हैं और निर्णय दिए जाते हैं। बल्कि आरोप ही अन्तिम निर्णय होते हैं। यह विचित्र अदालत है, जहाँ आपसे केवल सजा भुगतने की अपेक्षा की जाती है। ‘आत्मकथा’ एक शब्द भर है। यहाँ आत्मा को शक से देखा जाता है और कथ्य पर कोई भरोसा नहीं करता। जिस दिन कोई कह दे कि आप अपराधी हैं, बस उस दिन से आप अपराधी हैं।
लगातार सजा भुगतने की इस लेखकवाली जिंदगी में आप प्रायः जानना चाहते हैं कि आपका अपराध क्या है ? यह कोई नहीं बताएगा कि क्या विधान है, जिसका उल्लंघन करना दोष है। आपको पता लगेगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं, वही आपका अपराध है। हिन्दी में लेखक होने का अर्थ है, निरंतर कठघरे में खड़े रहना और वकीलों और न्यायधीशों की एक अनचाही, बिनबुलाई और प्रायः बदलती भीड़ द्वारा फतवे सुनना। आपकी यही नियति है। यह सब देख कर आपकी सिर पीटने की इच्छा होती है। उत्तेजित आप रहते हैं। अक्सर हिन्दी का ईमानदार लेखक भ्रम और उत्तेजना के बीच की जिंन्दगी जीता है। निराला सृजन के मामले में निराले थे, पर वे उदाहरण इसी तथ्य के हैं। जो तनिक भी निराले नहीं हैं, उदाहरण वे भी इसी परम तथ्य के हैं। अपना सिर पीटिए और यह जानने का प्रयत्न कीजिए कि लोग आपका सिर क्यों तोड़ने पर तुले हैं ? हिन्दी में लिखने का अर्थ निरंतर प्रहारों से सिर बचाना है, बेशर्मी से।
हिन्दी लेखक यानी सजायाफ्ता आदमी
इतने बरस हो गए कलम को कागज पर घिसते, मगर हिन्दी साहित्य के दफ्तर में मेरा पुराना आवेदन पत्र अभी भी विचारणीय स्थिति में अनिश्चितता की ट्रे में पड़ा है। मेरा आवेदन यह है कि कृपया मुझे लेखक मान लें। इस संदर्भ के लिए, मैं अपनी लिखी रचनाएँ प्रस्तुत करने को तैयार हूँ तथा नित नई लिखता रहता हूँ। मगर हिन्दी में लेखक कहलाने के लिए जिन कसौटियों पर आपकी जाँच होती है (और जाँचने की भी उन्हें कब फुरसत है ?) उनका लेखन से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे भोपाल के वे दिन याद हैं, जब मैं एक सरकारी अफसर से असहमत होने के कारण रातोंरात प्रतिक्रियावादी घोषित हो गया। फासिस्ट घोषित हो गया। मेरा सारा लिखा एक झटके में अकारथ हो गया। वह सारी कवि, लेखक, आलोचक वगैरह कहलानेवाली जमात, जो या तो स्वयं सरकारी नौकरी में थी या सत्ता से किसम-किसम के लाभ लेती थी, वह तो हुई प्रगतिशील, और मैं प्रतिक्रियावादी!
दोपहर को हलकी सी बहस हुई और कोई पाँच-साढ़े पाँच बजे ये नारे उछलने लगे कि मैं प्रतिक्रियावादी हूँ। सात बजे मुझे पता लगा। रात को अफसर के घर व्हिस्की की महफिल थी। उस रात यदि मैं उस महफिल में चला जाता और उसके चरणों पर सिर रख देता, तो सुबह तक फिर प्रगतिशील कहलाने लगता। मैं नहीं गया। सुबह पता लगा कि मैं अच्छा व्यंग्य लेखक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे व्यंग्य में हास्य ज्यादा होता है। मैंने सोचा, चलो हास्य सही। कुछ दिनों बाद मैंने अपना हास्य एकांकी प्रदर्शन के लिए दिया। समीक्षा और चर्चा में कहा गया कि एकांकी में हास्य नहीं है और वह एकांकी भी नहीं है। कर लो, क्या करते हो ?
मैं क्या कर सकता हूँ ? मैं एक और एकांकी लिखने का प्रयत्न कर सकता हूँ। वे मुझे लेखक न मानें, तो मैं सिवा और लिखने के क्या कर सकता हूँ ? बड़ी बेशर्मी-सी जिन्दगी है। यहाँ यशस्वी होना अनैतिक समझा जाता है। शाला में जब पढ़ता था और प्रतियोगिता जीत कर आता था, तो मेरे पिताजी ने कभी नहीं कहा कि बेटा, तुम गलत कर रहे हो। वे नासमझ रहे होंगे। हिन्दी की बारीकी नहीं समझते थे। बड़े होने पर पता लगा कि साहित्य की दृष्टि क्या है। जो रचना पाठकों द्वारा सराही गई, वही विद्वज्जनों को सतही और छिछली लगी। सस्ता यश पाने के लिए लिखी गई। थू-थू !
मेरा कसूर यह है कि लोग मुझे पढ़ते हैं। हिन्दी में पठनीय साहित्य, साहित्य नहीं होता। वह कुछ भ्रष्ट और सतही चीज होती है। मैं बहुत शुरू से उन पत्र-पत्रिकाओं में लिखने लगा, जिनकी बिक्री ज्यादा थी, जो ज्यादा पाठकों से जुड़ती थीं। साहित्य के मठाधीश यह आग्रह करेंगे कि आपका लेखन जनता से जुड़े, पर यदि आप ऐसी पत्रिका में लिख रहे हैं, जो ज्यादा बिकती है, तो वे आप पर भी नाक-भौं सिकोड़ेंगे। हिन्दी में लोकप्रिय होना अपराध है। जो नहीं पढ़े जाते, वे ही लेखक हैं, और जो नापसंद किए जाते हैं, वे बेहतर लेखक हैं। यहाँ तक भी ठीक है। पर जो पढ़े जाते हैं, वे लेखक हैं ही नहीं। जो कवि मंच पर पढ़ता है, वह कवि नहीं। दिल्ली के एक हॉल में कुछ लोगों को जमा कर के अपनी कविताएँ अज्ञेय भी पढ़ते हैं, पर यदि वही हॉल कुछ और चौड़ा हो जाए, सुननेवालों की संख्या चौगुनी हो जाए और कोई कवि पढ़ रहा हो, प्रशंसा पा रहा हो, तो वह कवि नहीं है। किसी भी भाषा में लेखक का समाज से जुड़ना घटिया प्रवृत्ति नहीं समझी जाती, सिवा हिन्दी के।
मैं पुराना अपराधी हूँ और वर्षों से साहित्यवालों की घृणा का पात्र हूँ। कॉलेज के दिनों में मैं रचना के पारिश्रमिक से अपनी पढ़ाई का खर्च चलाता था। जब भी मनीऑर्डर आता, मैं प्रसन्न होता था। बाद में पता लगा कि यह प्रसन्नता अपराध है। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद लेखन के सहारे मेरा काम चला। मैं भोपाल में सरकार के चरणों में सिर टेके बिना जी लिया। मेरे लिए लिखना और उसका चेक या मनीऑर्डर लेना एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। यह अपराध है। मैं व्यावसायिक लेखक हूँ, अतः घटिया हूँ। साहित्य वाले मेरी रचना नहीं पढ़ेंगे। चूँकि मैं व्यावसायिक पत्रों में नियमित लिखकर कमाता हूँ, अतः मैं कोई दर्जा नहीं रखता। दर्जेदार वे हैं, जो विश्वविद्यालय की पीठ पर विराजमान हो, बिना पढ़ाए मुफ्त का पैसा झाड़, साहित्य और साहित्यकार पर फतवे देते हैं। पद, पुरस्कार और पद्मश्री तक, सारा कुछ बटोरने के उपक्रम में सरकार के विरुद्ध लिखने से कतरा कर, मार्क्सवादी बनते हैं। अपनी तुलना कबीर से करेंगे और अपनी चदरिया मुख्यमंत्री के चरणों में बिछाये रखेंगे। शिखर का पुरस्कार लेने के लिए जमीन पर बिछ जाएँगे। सरकार से खरीदी करवा लेने का लालच दे, छुटभैयों से अपने पर किताब लिखवायेंगे, ग्रंथावली का जुगाड़ जमाएँगे।
दोपहर को हलकी सी बहस हुई और कोई पाँच-साढ़े पाँच बजे ये नारे उछलने लगे कि मैं प्रतिक्रियावादी हूँ। सात बजे मुझे पता लगा। रात को अफसर के घर व्हिस्की की महफिल थी। उस रात यदि मैं उस महफिल में चला जाता और उसके चरणों पर सिर रख देता, तो सुबह तक फिर प्रगतिशील कहलाने लगता। मैं नहीं गया। सुबह पता लगा कि मैं अच्छा व्यंग्य लेखक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे व्यंग्य में हास्य ज्यादा होता है। मैंने सोचा, चलो हास्य सही। कुछ दिनों बाद मैंने अपना हास्य एकांकी प्रदर्शन के लिए दिया। समीक्षा और चर्चा में कहा गया कि एकांकी में हास्य नहीं है और वह एकांकी भी नहीं है। कर लो, क्या करते हो ?
मैं क्या कर सकता हूँ ? मैं एक और एकांकी लिखने का प्रयत्न कर सकता हूँ। वे मुझे लेखक न मानें, तो मैं सिवा और लिखने के क्या कर सकता हूँ ? बड़ी बेशर्मी-सी जिन्दगी है। यहाँ यशस्वी होना अनैतिक समझा जाता है। शाला में जब पढ़ता था और प्रतियोगिता जीत कर आता था, तो मेरे पिताजी ने कभी नहीं कहा कि बेटा, तुम गलत कर रहे हो। वे नासमझ रहे होंगे। हिन्दी की बारीकी नहीं समझते थे। बड़े होने पर पता लगा कि साहित्य की दृष्टि क्या है। जो रचना पाठकों द्वारा सराही गई, वही विद्वज्जनों को सतही और छिछली लगी। सस्ता यश पाने के लिए लिखी गई। थू-थू !
मेरा कसूर यह है कि लोग मुझे पढ़ते हैं। हिन्दी में पठनीय साहित्य, साहित्य नहीं होता। वह कुछ भ्रष्ट और सतही चीज होती है। मैं बहुत शुरू से उन पत्र-पत्रिकाओं में लिखने लगा, जिनकी बिक्री ज्यादा थी, जो ज्यादा पाठकों से जुड़ती थीं। साहित्य के मठाधीश यह आग्रह करेंगे कि आपका लेखन जनता से जुड़े, पर यदि आप ऐसी पत्रिका में लिख रहे हैं, जो ज्यादा बिकती है, तो वे आप पर भी नाक-भौं सिकोड़ेंगे। हिन्दी में लोकप्रिय होना अपराध है। जो नहीं पढ़े जाते, वे ही लेखक हैं, और जो नापसंद किए जाते हैं, वे बेहतर लेखक हैं। यहाँ तक भी ठीक है। पर जो पढ़े जाते हैं, वे लेखक हैं ही नहीं। जो कवि मंच पर पढ़ता है, वह कवि नहीं। दिल्ली के एक हॉल में कुछ लोगों को जमा कर के अपनी कविताएँ अज्ञेय भी पढ़ते हैं, पर यदि वही हॉल कुछ और चौड़ा हो जाए, सुननेवालों की संख्या चौगुनी हो जाए और कोई कवि पढ़ रहा हो, प्रशंसा पा रहा हो, तो वह कवि नहीं है। किसी भी भाषा में लेखक का समाज से जुड़ना घटिया प्रवृत्ति नहीं समझी जाती, सिवा हिन्दी के।
मैं पुराना अपराधी हूँ और वर्षों से साहित्यवालों की घृणा का पात्र हूँ। कॉलेज के दिनों में मैं रचना के पारिश्रमिक से अपनी पढ़ाई का खर्च चलाता था। जब भी मनीऑर्डर आता, मैं प्रसन्न होता था। बाद में पता लगा कि यह प्रसन्नता अपराध है। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद लेखन के सहारे मेरा काम चला। मैं भोपाल में सरकार के चरणों में सिर टेके बिना जी लिया। मेरे लिए लिखना और उसका चेक या मनीऑर्डर लेना एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। यह अपराध है। मैं व्यावसायिक लेखक हूँ, अतः घटिया हूँ। साहित्य वाले मेरी रचना नहीं पढ़ेंगे। चूँकि मैं व्यावसायिक पत्रों में नियमित लिखकर कमाता हूँ, अतः मैं कोई दर्जा नहीं रखता। दर्जेदार वे हैं, जो विश्वविद्यालय की पीठ पर विराजमान हो, बिना पढ़ाए मुफ्त का पैसा झाड़, साहित्य और साहित्यकार पर फतवे देते हैं। पद, पुरस्कार और पद्मश्री तक, सारा कुछ बटोरने के उपक्रम में सरकार के विरुद्ध लिखने से कतरा कर, मार्क्सवादी बनते हैं। अपनी तुलना कबीर से करेंगे और अपनी चदरिया मुख्यमंत्री के चरणों में बिछाये रखेंगे। शिखर का पुरस्कार लेने के लिए जमीन पर बिछ जाएँगे। सरकार से खरीदी करवा लेने का लालच दे, छुटभैयों से अपने पर किताब लिखवायेंगे, ग्रंथावली का जुगाड़ जमाएँगे।
नमक-मिर्च लगी आलोचना
हिन्दी में ऐसे ही पाखंडियों का साम्राज्य है। संस्थाएँ बना कर फोर्ड फाउंडेशन से लेकर राज्य सरकार तक से पैसा झटक कर भ्रष्ट कर्मों में लिप्त लोगों की विराट् दुनिया है। आपको उसी में रहना और उसे सहन करना है। लेखक के नाते मैं इस देश की किसी भी दुष्प्रवत्ति पर कमेंट कर सकता हूँ, पर हिन्दी में चलनेवाली इन दुष्ट गतिविधियों पर नहीं। फौरन सरलीकरण हो जाएगा। जोशी जी को पुरस्कार नहीं मिला ना, इसलिए जलते हैं। सरकार ने जोशी जी की किताब नहीं खरीदी इसलिए दुखी हैं। आप जरा सच बोल दीजिए, फौरन सुनने को मिलेगा—फ्रस्ट्रेटेड हैं। इनकी कुंठाएँ बोल रही हैं। हिन्दी में लेखक होने का अर्थ पता नहीं ऐसे कितने सरलीकरणों का शिकार होना है। लेखन से भी बड़ी हॉबी है यहाँ, दूसरों के ईमान पर संदेह करना और उस संदेह को निहायत अस्वस्थ तरीके से व्यक्त करना।
जब गद्य लेखन में मेरी रुचि बढ़ी, अर्थात् सन्’ 48 के बाद अपेक्षाकृत तेजी से, उन दिनों मैंने जिन लेखकों को पढ़ा, वे थे चेखव, यशपाल, गोर्की, मोपासां, बालजक, प्रेमचंद, ओ‘हेनरी, कृश्नचंदर, मंटो, शरत, रवीन्द्र, सॉमरसेट मॉम और तॉल्सतॉय। इनमें तॉल्सतॉय को अपनी खानदानी जमीन से कुछ वार्षिक कमाई होती थी। शेष सारे लेखकों के विषय में मुझे यह सोच ठीक ही लगता था कि उनकी जीविका लिखने से चलती है। मैंने तब सोचा, क्यों नहीं मैं भी लिख कर ही जीऊँ ? उन दिनों येन-केन प्रकारेण लखपती बनने के दिल्ली-पंजाबी मूल्य हमारे देश पर छाए नहीं थे। मैं मालवा के एक मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार का लड़का, इससे अधिक सोचता भी क्या ? और दस वर्ष भी लिखते न गुजरे होंगे कि हिन्दी में आंदोलन चला कि व्यावसायिक पत्रिकाओं में लिखना पाप है। यह आंदोलन उन प्राध्यापकों ने चलाया था, जिनकी तनख्वाह विश्वविद्यालय आयोग के नए जोरदार वेतनमानों के कारण तेजी से एकाएक बढ़ गयी थी। मैं ‘धर्मयुग’ और ‘सारिका’ में लिखता था और लिखना न छोड़ सकता था, न छोड़ना चाहता था। मैं फौरन अछूत घोषित हो गया और वे सब मेरे बेटे उच्च ब्राह्मण हो गये। जरा सोचिए, ‘जब मैं ‘नई दुनिया’ इंदौर में सप्ताह में तीन की गति से कॉलम लिखता था, मुझे तीस रुपये प्रति महीने मिलते थे अर्थात् माह में बारह कालम के प्रति कॉलम ढाई रुपये। कहानी लिखने पर बारह रुपये से बीस रुपये तक प्राप्त होते थे। यह 1952-54 की बात है। तब मेरा प्रतिदिन का खर्च था एक रुपया। इसमें दो तीन दिन का खर्च बचाकर एकाध किताब खरीद लेने की एय्याशी भी शामिल थी। आज तीस वर्ष बाद हिन्दी की नामी-गिरामी पत्रिकाएँ एक लेख का पेमेंट डेढ़ सौ से ढाई सौ तक करती हैं। मतलब आप तीस साल में ढाई रुपये से अधिक ढाई सौ तक पहुँचे और सुखी जीवन, अर्थात् दाल-रोटी की सुनिश्चितता के लिए सप्ताह में तीन बार आज भी लिखना जरूरी है।
जब गद्य लेखन में मेरी रुचि बढ़ी, अर्थात् सन्’ 48 के बाद अपेक्षाकृत तेजी से, उन दिनों मैंने जिन लेखकों को पढ़ा, वे थे चेखव, यशपाल, गोर्की, मोपासां, बालजक, प्रेमचंद, ओ‘हेनरी, कृश्नचंदर, मंटो, शरत, रवीन्द्र, सॉमरसेट मॉम और तॉल्सतॉय। इनमें तॉल्सतॉय को अपनी खानदानी जमीन से कुछ वार्षिक कमाई होती थी। शेष सारे लेखकों के विषय में मुझे यह सोच ठीक ही लगता था कि उनकी जीविका लिखने से चलती है। मैंने तब सोचा, क्यों नहीं मैं भी लिख कर ही जीऊँ ? उन दिनों येन-केन प्रकारेण लखपती बनने के दिल्ली-पंजाबी मूल्य हमारे देश पर छाए नहीं थे। मैं मालवा के एक मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार का लड़का, इससे अधिक सोचता भी क्या ? और दस वर्ष भी लिखते न गुजरे होंगे कि हिन्दी में आंदोलन चला कि व्यावसायिक पत्रिकाओं में लिखना पाप है। यह आंदोलन उन प्राध्यापकों ने चलाया था, जिनकी तनख्वाह विश्वविद्यालय आयोग के नए जोरदार वेतनमानों के कारण तेजी से एकाएक बढ़ गयी थी। मैं ‘धर्मयुग’ और ‘सारिका’ में लिखता था और लिखना न छोड़ सकता था, न छोड़ना चाहता था। मैं फौरन अछूत घोषित हो गया और वे सब मेरे बेटे उच्च ब्राह्मण हो गये। जरा सोचिए, ‘जब मैं ‘नई दुनिया’ इंदौर में सप्ताह में तीन की गति से कॉलम लिखता था, मुझे तीस रुपये प्रति महीने मिलते थे अर्थात् माह में बारह कालम के प्रति कॉलम ढाई रुपये। कहानी लिखने पर बारह रुपये से बीस रुपये तक प्राप्त होते थे। यह 1952-54 की बात है। तब मेरा प्रतिदिन का खर्च था एक रुपया। इसमें दो तीन दिन का खर्च बचाकर एकाध किताब खरीद लेने की एय्याशी भी शामिल थी। आज तीस वर्ष बाद हिन्दी की नामी-गिरामी पत्रिकाएँ एक लेख का पेमेंट डेढ़ सौ से ढाई सौ तक करती हैं। मतलब आप तीस साल में ढाई रुपये से अधिक ढाई सौ तक पहुँचे और सुखी जीवन, अर्थात् दाल-रोटी की सुनिश्चितता के लिए सप्ताह में तीन बार आज भी लिखना जरूरी है।
सतत लेखन बनाम स्तरहीनता का आरोप
यदि आपकी किताब बराबर बिकती नहीं है, तो डेढ़ सौ पृष्ठ की पुस्तक पर साल भर में रॉयल्टी होगी अधिक-से-अधिक बारह सौ अर्थात् सौ रुपया प्रति माह। उसमें ओढ़-बिछा लीजिए। पर यदि आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं, अर्थात् निरंतर लिख रहे हैं, तो साहित्य वाले अपनी व्हिस्की के गिलास में बर्फ का टुकड़ा डालते हुए कहेंगे, निरंतर लिखने से शरद जी की राइटिंग में वह स्तरीयता नहीं है।’ सरलता से कह दी जाएगी बात। हिन्दी में सक्रिय लेखन कार्य का अर्थ है स्तरहीन लेखन। जो दादूराम महीनों बिना लिखे, दूतावासों में घुसपैठ कर विदेश यात्राओं का डौल जमाते हैं। वे हैं स्तरीय लेखक। यदि प्रसिद्ध इतिहास लेखक होते, तो यहाँ उनका पत्थरों से सिर फोड़ दिया जाता। वे रोज सुबह साढ़े नौ बजे अपनी लिखने की मेज पर आ जाते हैं और पाँच बजे तक लिखते रहते हैं या फिर पिछले लिखे को दुरुस्त करते रहते हैं। हिन्दी में होते तो कभी के स्तरहीन घोषित कर दिए जाते।
मैं अपराधी हूँ। स्तरहीन हूँ। व्यावसायिक हूँ। यश कमाने का गुनाह किया है मैंने। मेरा अपराध यह है कि मैंने लिखने के काम को अपने जीवन से जोड़ लिया है। मैं कई रेडियो-वार्ताएँ और लेख इसलिए लिखे हैं कि मुझे फौरन पच्चीस-पचास रुपये की आवश्यकता थी। मैंने यह किया और मुझे इसकी कोई शर्म नहीं है। लिखने का मेरे जीवन में सबसे बड़ा महत्व यही है कि लेखन ने मुझे आत्महत्या से बचाया, भूखे रहने से बचाया, नंगे रहने से बचाया। मैं रचना का पेमेंट जेब में रख कर कॉफी हाउस में घुसा हूँ, बुश्शर्ट खरीदने निकला हूँ। मैंने लिखकर निजी जरूरतें पूरी की हैं।
हिन्दी में लिखने का अर्थ है, साहित्यवालों द्वारा दिए कांप्लेक्स का शिकार होना। आप जो कर रहे हैं, जिसे करने में आप जीवन की सार्थकता अनुभव करते हैं, आपका वही गुण हिन्दी में आपका काप्लेक्स बन जाएगा। आप फिर भी वही करेंगे, अर्थात् आप बेशर्मी अख्तियार करेंगे, तभी आप लिख सकेंगे। यहाँ यह कहने वालों की कमी तो है ही नहीं कि आप गलत लिख रहे हैं। ऐसे भी कम नहीं, जो आपको उस रास्ते से हटा दें। उनका शत्रु वह है, जो उनके चाहे रास्ते से नहीं हटता।
भोपाल में एक अफसर से झगड़ा होने के बाद मुझे झुकाने के लिए साजिश की तरह मेरी आय के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। मैंने तय किया चलो, बंबई चलें। वहाँ लिखेंगे। अखबारों में लिखेंगे, फिल्मों के लिए लिखेंगे। उस शाम मैं कॉफीहाउस में बैठा था। एक उदीयमान किस्म के कवि-आलोचक ने मुझसे पूछा, ‘शरद जी, अब तो बंबई जा रहे हैं। अब तो आपका लिखना समाप्त हो जाएगा।’ मैंने कहा, ‘समाप्त तो नहीं होगा, हाँ कम हो जाएगा। फिर भी तुम साल भर में मिल कर जितना लिखते हो, उससे मैं अधिक ही लिखूँगा।’ मतलब यदि आप बंबई जा रहे हैं। हें-हें। हम बेहतर लेखक हैं। हम सागर जा रहे हैं।
आप हिन्दी में कलम चलाते हैं, तो आपकी भावना प्रायः होती है कि आप जूता मारे खींच कर। निरंतर सहन करने का नाम हिन्दी लेखक होना है। कई बार यही सहनशीलता और चुप्पी एक ग्रंथि बन जाती है। उसे तोड़ते रहना पड़ता है। इसके बिना लिखना और जीना, दोनों कठिन हैं।
लिखने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी-सी धूप, ठंडी हवा, बढ़िया कागज और एक ऐसी कलम, जो बीच में न रुके। एकाध चाय। मैं आपको एक सुन्दर रचना देने का वादा करता हूँ। पर इस धूप की गारंटी नहीं है हिन्दी में। कितनी बार, कितने घर, कितने कमरे, कितने आँगन बदलता हुआ मैं आज भी अपने जीवन को लेकर अनिश्चित हूँ। इस भाषा में केवल हत्याकांड होते हैं। यहाँ जीवन जीने की साफ-सुथरी स्थिति नहीं मिलती। और मैं चूँकि व्यंग्य लिखता हूँ, इसलिए मेरे लिए तो ऐसी स्थिति नहीं मिलने का प्रश्न ही नहीं है। लिखना पूर्वजन्म का कोई दंड झेलना है। इसे निरंतर झेले बिना इससे मुक्ति नहीं। मैं झेल रहा हूँ। पर मुझसे कहा जाए कि इस जन्म में भी आप पाप कर रहे हैं, तो यह मुझे स्वीकार नहीं।
मैं अब महज लेखक हूँ। शेष जीवन भी रहूँगा। मैं कर्तव्यवश, जीवन जीने के लिए, एक आदमी की तरह, जो अपने समाज और देश के सुख-दुख में बतौर नागरिक हिस्सेदारी करता है, रोटी कमाता है, बीमारी सहता है। हँसता है, मिलता है, मजे लेता है, यात्राएँ करता है, बातें करता है, यह जानते हुए कि ऐसा ही करते हुए उसे जल्दी या देर से कभी मर जाना है, वह रोज अखबार पढ़े बिना नहीं रहता, अपने गुण-दोष के साथ जीता है। मैं हिन्दी साहित्य की दुनिया का नागरिक कतई नहीं हूँ। उसे उन्हीं चरणों में पड़ी रहने दो, जहाँ वह पड़ी है। वही शायद उसका लक्ष्य था। दरबारों से निकली और दरबार में घुस गई। मैं अपने फुटपाथ पर चला हूँ। मैं उसकी स्थिति बदलने के लिए भी कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझसे बेहतर प्रज्ञा के सजग, सचेत, समझदार और कमिटेड किस्म के लोग उसे दरबार में ले जाने में लगे हैं। मैं उनसे पराजित हूँ।
मैं अपराधी हूँ। स्तरहीन हूँ। व्यावसायिक हूँ। यश कमाने का गुनाह किया है मैंने। मेरा अपराध यह है कि मैंने लिखने के काम को अपने जीवन से जोड़ लिया है। मैं कई रेडियो-वार्ताएँ और लेख इसलिए लिखे हैं कि मुझे फौरन पच्चीस-पचास रुपये की आवश्यकता थी। मैंने यह किया और मुझे इसकी कोई शर्म नहीं है। लिखने का मेरे जीवन में सबसे बड़ा महत्व यही है कि लेखन ने मुझे आत्महत्या से बचाया, भूखे रहने से बचाया, नंगे रहने से बचाया। मैं रचना का पेमेंट जेब में रख कर कॉफी हाउस में घुसा हूँ, बुश्शर्ट खरीदने निकला हूँ। मैंने लिखकर निजी जरूरतें पूरी की हैं।
हिन्दी में लिखने का अर्थ है, साहित्यवालों द्वारा दिए कांप्लेक्स का शिकार होना। आप जो कर रहे हैं, जिसे करने में आप जीवन की सार्थकता अनुभव करते हैं, आपका वही गुण हिन्दी में आपका काप्लेक्स बन जाएगा। आप फिर भी वही करेंगे, अर्थात् आप बेशर्मी अख्तियार करेंगे, तभी आप लिख सकेंगे। यहाँ यह कहने वालों की कमी तो है ही नहीं कि आप गलत लिख रहे हैं। ऐसे भी कम नहीं, जो आपको उस रास्ते से हटा दें। उनका शत्रु वह है, जो उनके चाहे रास्ते से नहीं हटता।
भोपाल में एक अफसर से झगड़ा होने के बाद मुझे झुकाने के लिए साजिश की तरह मेरी आय के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। मैंने तय किया चलो, बंबई चलें। वहाँ लिखेंगे। अखबारों में लिखेंगे, फिल्मों के लिए लिखेंगे। उस शाम मैं कॉफीहाउस में बैठा था। एक उदीयमान किस्म के कवि-आलोचक ने मुझसे पूछा, ‘शरद जी, अब तो बंबई जा रहे हैं। अब तो आपका लिखना समाप्त हो जाएगा।’ मैंने कहा, ‘समाप्त तो नहीं होगा, हाँ कम हो जाएगा। फिर भी तुम साल भर में मिल कर जितना लिखते हो, उससे मैं अधिक ही लिखूँगा।’ मतलब यदि आप बंबई जा रहे हैं। हें-हें। हम बेहतर लेखक हैं। हम सागर जा रहे हैं।
आप हिन्दी में कलम चलाते हैं, तो आपकी भावना प्रायः होती है कि आप जूता मारे खींच कर। निरंतर सहन करने का नाम हिन्दी लेखक होना है। कई बार यही सहनशीलता और चुप्पी एक ग्रंथि बन जाती है। उसे तोड़ते रहना पड़ता है। इसके बिना लिखना और जीना, दोनों कठिन हैं।
लिखने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी-सी धूप, ठंडी हवा, बढ़िया कागज और एक ऐसी कलम, जो बीच में न रुके। एकाध चाय। मैं आपको एक सुन्दर रचना देने का वादा करता हूँ। पर इस धूप की गारंटी नहीं है हिन्दी में। कितनी बार, कितने घर, कितने कमरे, कितने आँगन बदलता हुआ मैं आज भी अपने जीवन को लेकर अनिश्चित हूँ। इस भाषा में केवल हत्याकांड होते हैं। यहाँ जीवन जीने की साफ-सुथरी स्थिति नहीं मिलती। और मैं चूँकि व्यंग्य लिखता हूँ, इसलिए मेरे लिए तो ऐसी स्थिति नहीं मिलने का प्रश्न ही नहीं है। लिखना पूर्वजन्म का कोई दंड झेलना है। इसे निरंतर झेले बिना इससे मुक्ति नहीं। मैं झेल रहा हूँ। पर मुझसे कहा जाए कि इस जन्म में भी आप पाप कर रहे हैं, तो यह मुझे स्वीकार नहीं।
मैं अब महज लेखक हूँ। शेष जीवन भी रहूँगा। मैं कर्तव्यवश, जीवन जीने के लिए, एक आदमी की तरह, जो अपने समाज और देश के सुख-दुख में बतौर नागरिक हिस्सेदारी करता है, रोटी कमाता है, बीमारी सहता है। हँसता है, मिलता है, मजे लेता है, यात्राएँ करता है, बातें करता है, यह जानते हुए कि ऐसा ही करते हुए उसे जल्दी या देर से कभी मर जाना है, वह रोज अखबार पढ़े बिना नहीं रहता, अपने गुण-दोष के साथ जीता है। मैं हिन्दी साहित्य की दुनिया का नागरिक कतई नहीं हूँ। उसे उन्हीं चरणों में पड़ी रहने दो, जहाँ वह पड़ी है। वही शायद उसका लक्ष्य था। दरबारों से निकली और दरबार में घुस गई। मैं अपने फुटपाथ पर चला हूँ। मैं उसकी स्थिति बदलने के लिए भी कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझसे बेहतर प्रज्ञा के सजग, सचेत, समझदार और कमिटेड किस्म के लोग उसे दरबार में ले जाने में लगे हैं। मैं उनसे पराजित हूँ।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book