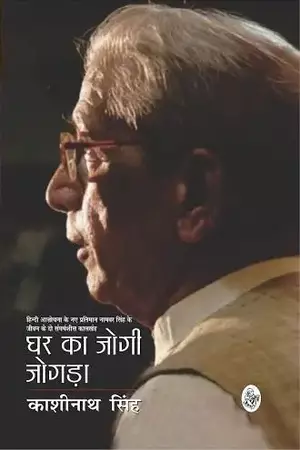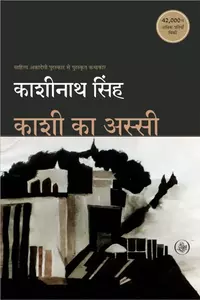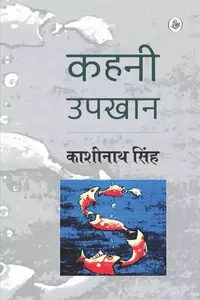|
संस्मरण >> घर का जोगी जोगड़ा घर का जोगी जोगड़ाकाशीनाथ सिंह
|
405 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है काशीनाथ सिंह का संस्मरण
ghar ka jogi jogra
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘गरबीली गरीबी वह’ के बारे में
‘अद्भुत रचना है काशी का संस्मरण-जिस ऊष्मा, सम्मान और समझदार संयम से लिखा गया है, वह पहली बार तो अभिभूति कर लेता है। मैं इसे नामवरी सठियाना-समारोह की एक उपलब्धि मानता हूँ। साथ ही मेरी यह राय भी है कि अगर ऐसी कलम हो तो हिटलर को भी भगवान बुद्ध का अवतार बनाकर पेश किया जा सकता है। (मज़ाक अलग) व्यक्तित्व के अन्तर्विरोधों पर भी कुछ बात की जाती तो शायद और ज़्यादा जीवन्त संस्मरण होता !
‘घर का जोगी जोगड़ा’ के बारे में
‘काशीनाथ सिंह का आख्यानक उनके रचनात्मक गद्य की पूरी ताकत के साथ सामने आया है। काशी के पास रचानात्मक गद्य की जीवंतता है-गहरे अनुभव-संवेदन हैं। उनकी भाषा को लेकर और अभिव्यक्ति भंगिमाओं को लेकर काफी कुछ कहा गया है, परन्तु जो बात देखने की है वह यह है कि अपनी जमीन और परिवेश से काशी बना देने का कितना माद्दा है। काशी पूरी ऊर्जा में बहुत सहज होकर लिखते हैं और जब ‘भइया’ सामने हों तो वे अपनी रचनात्मकता के चरम पर पहुँचते हैं और महत्त्वपूर्ण के साथ-साथ तमाम मार्मिक और बेधक भी हमें दे जाते हैं।
बहुपठित, बहुचर्चित, बहुप्रशंसित संस्मरण हैं ये कथाकार भाई काशीनाथ सिंह के। केन्द्र में हैं हिंदी समीक्षा के शिखर पुरुष नामवर सिंह के जीवन के अलग-अलग दो संघर्षशील कालखंड ! विशेष बात सिर्फ यह कि यदि ‘गरबीली गरीबी वह’ ने संस्करण विधा को पुनर्जीवन के साथ पहचान दी थी तो ‘घर का जोगी जोगड़ा’ ने उसे नई ऊँचाई और सम्भावनाएँ।
वे (नामवर) हिन्दी के पहले मिशनरी आलोचक हुए जो साहित्य की चिन्ताओं के साथ हिन्दी और अहिन्दी प्रदेश के शहरों में ही नहीं, कस्बों और गाँवों तक गए; ज्ञानियों, अज्ञानियों, और विज्ञानियों के बीच गए, पढ़े-लिखों और बेपढ़ों को सुना-सुनाया, हिलाया-झुकाया, झकझोरा उसके बीच बोलकर जो साहित्य से बाहर के थे, गैर-पेशे के थे और हिन्दी और साहित्य के प्रति उपहास का भाव रखते थे ! उन्होंने उनके भीतर एक बेचैनी पैदा की-जीवन के लिए, समाज के लिए; और अहसास कराया कि साहित्य वही नहीं है जो किताबों में हैं, और जो किताबों में है वह भी तुम्हारे जीवन और साहित्य के सिवा कुछ दूसरा नहीं है। किताबों से बाहर जो तुम्हारे खाने-पीने और जीने-मरने में है वह भी साहित्य है।
पचासों हैं जिनमें कविता-कहानी का विवेक नामवर को सुनकर आया है।
सैकड़ों हैं जिन्होंने कोई कविता इसलिए खरीदी कि उसका जिक्र नामवर के व्याख्यान में आया था।
हजारों हैं जिनकी साहित्य में दिलचस्पी नामवार को सुनकर हुई है।
और ऐसे संख्या तो लाखों में हैं जिन्हें नामवर को सुनकर हिन्दी स्वादिष्ट लगी है। इसी को नामवर आलोचना की ‘वाचिक परम्परा’ कहते हैं....
बहुपठित, बहुचर्चित, बहुप्रशंसित संस्मरण हैं ये कथाकार भाई काशीनाथ सिंह के। केन्द्र में हैं हिंदी समीक्षा के शिखर पुरुष नामवर सिंह के जीवन के अलग-अलग दो संघर्षशील कालखंड ! विशेष बात सिर्फ यह कि यदि ‘गरबीली गरीबी वह’ ने संस्करण विधा को पुनर्जीवन के साथ पहचान दी थी तो ‘घर का जोगी जोगड़ा’ ने उसे नई ऊँचाई और सम्भावनाएँ।
वे (नामवर) हिन्दी के पहले मिशनरी आलोचक हुए जो साहित्य की चिन्ताओं के साथ हिन्दी और अहिन्दी प्रदेश के शहरों में ही नहीं, कस्बों और गाँवों तक गए; ज्ञानियों, अज्ञानियों, और विज्ञानियों के बीच गए, पढ़े-लिखों और बेपढ़ों को सुना-सुनाया, हिलाया-झुकाया, झकझोरा उसके बीच बोलकर जो साहित्य से बाहर के थे, गैर-पेशे के थे और हिन्दी और साहित्य के प्रति उपहास का भाव रखते थे ! उन्होंने उनके भीतर एक बेचैनी पैदा की-जीवन के लिए, समाज के लिए; और अहसास कराया कि साहित्य वही नहीं है जो किताबों में हैं, और जो किताबों में है वह भी तुम्हारे जीवन और साहित्य के सिवा कुछ दूसरा नहीं है। किताबों से बाहर जो तुम्हारे खाने-पीने और जीने-मरने में है वह भी साहित्य है।
पचासों हैं जिनमें कविता-कहानी का विवेक नामवर को सुनकर आया है।
सैकड़ों हैं जिन्होंने कोई कविता इसलिए खरीदी कि उसका जिक्र नामवर के व्याख्यान में आया था।
हजारों हैं जिनकी साहित्य में दिलचस्पी नामवार को सुनकर हुई है।
और ऐसे संख्या तो लाखों में हैं जिन्हें नामवर को सुनकर हिन्दी स्वादिष्ट लगी है। इसी को नामवर आलोचना की ‘वाचिक परम्परा’ कहते हैं....
-इसी पुस्तक से....
बाबा जोगी एक अकेला।
जाके तीरथ बरत न मेला।।
झोली पत्र भभूत न बटुवा,
अनहद बेन बजावै।
माँगि न खाइ न भूखा सोवै,
घर अँगना फिरि आवै।
पाँच जना क जमात चलावै,
तास गुरू मैं चेला।
कहै कबीर उनि देस सिधाया।
बहुरि न इह जग मेला।।
बाबा जोगी एक अकेला।।
(‘कबीर-समग्र’ पद, पृ.609)
जाके तीरथ बरत न मेला।।
झोली पत्र भभूत न बटुवा,
अनहद बेन बजावै।
माँगि न खाइ न भूखा सोवै,
घर अँगना फिरि आवै।
पाँच जना क जमात चलावै,
तास गुरू मैं चेला।
कहै कबीर उनि देस सिधाया।
बहुरि न इह जग मेला।।
बाबा जोगी एक अकेला।।
(‘कबीर-समग्र’ पद, पृ.609)
स्मरण
शायद ही मेरी कोई ऐसी कहानी हो जो भैया को पसन्द हो लेकिन ऐसा संस्मरण और कथा-रिपोर्ताज भी शायद ही हो जो उन्हें नापसन्द हो।
यह कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि वे मेरे बड़े भाई ही नहीं, कथागुरु भी हैं। मुझमें जो भी थोड़ा-बहुत कथा-विवेक है, उन्हीं से अर्जित है। अगर मैं कहानी से संस्मरण की तरफ गया और फिर संस्मरण से कथा-रिपोर्ताज की ओर—तो इसके पीछे कहीं न कहीं वे भी हैं। उनके सिवा और कौन समझ सकता है कि मेरे कथकार की कमजोरियों और उसकी रचनात्मक ताकत को ? लम्बे-चौड़े मैदान में एक ही स्थान पर खड़े रहकर जिन्दगी भर ‘बाएँ-दाएँ’ करते रहने से बेहतर है अपनी सम्भावनाओं और क्षमताओं के लिए नए क्षितिज खोजना और किसी ऊसर पड़े खेत को हरा-भरा बनाना !
मैं उन्हें अपने कानों से पढ़ता रहा हूँ पिछले पचास वर्षों से। वे जो कहते रहते हैं, उसे कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते। ऐसा भी हुआ है कि जिस बात को सन् ’60 से कहते रहे हों, उसे 90 में जाकर लिखा हो। मैं जिस नगर में रहता हूँ वह मूल रूप से स्मृति और श्रुतिपरम्परा का ही नगर है। मुझे कहने में संकोच नहीं कि मैंने उन्हें कम से कम पढ़ा है और समझा तो उससे भी कम। लेकिन उनसे जो सुनता हूँ उनमें से अपने काम की या जरूरत की बातें गिरह बाँध लेता हूँ।
मुझे अपना पहला संस्मरण लिखना पड़ा उनकी ‘षष्टिपूर्ति पर ! ‘पहल’ के लिए ! यानी ’85-’86 के करीब ! कहानियाँ लिखते-लिखते ऊब-सा रहा था। कहानी से जो चाहता था, वह नहीं हो रहा था मुझसे। और संस्मरण के लिए हिन्दी में कोई मॉडल नहीं था मेरे सामने ! जो था वह रूखा, सूखा बेजान, अनाकर्षक, मांस-मज्जा हीन, ऊष्मा रहित। हड्डियों के निर्जीव ढाँचे की तरह। साथ ही संस्मरण की जगह साहित्य के समाज में उस दलित जैसी थी जिसके लिए ‘पंगत’ में कोई पत्तल नहीं।
मेरा कथाकार संस्मरण के शास्त्र को बदल देना चाहता था लेकिन यह उस पर नहीं, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के जीवन पर निर्भर था जो जीने की निर्धारित शास्त्रीयता को अस्वीकार कर रहे थे !
मुझे याद आया भैया का एक पत्र। सन् ’65 में बनारस छोड़ने के बाद का पहला पत्र। दिल्ली से। मुक्तिबोध को गुजरे कुछ ही महीने हो रहे थे और उन पर ‘राष्ट्रवाणी’ का एक अंक आया था। पत्र के अन्त में उन्होंने दो वाक्य लिखे थे-‘तुमने ‘राष्ट्रवाणी’ के मुक्तिबोध विशेषांक में छोटे भाई शरत मुक्तिबोध का निबंध पढ़ा ? पढ़ लेना, कौन जाने कभी तुम्हें भी लिखना पड़े तब याद रखना कि गद्य ऐसा ही हो-बल्कि इससे भी ज़्यादा खुश्क ! मैंने वह संस्मरण पढ़ा था लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं लगा था। इस चिट्ठी में मेरे मतलब की सिर्फ एक चीज़ थी कि गद्य कैसा हो ? खुश्क यानी गीला न हो, भीगा न हो-कपड़े उसे निचोड़ कर, पानी निथार कर सुखा लो और जब हल्का, कड़कड़ हो जाए, उसमें चमक आ जाए तब इस्तेमाल करो। राग-विराग मुक्त गद्य ! यह मेरी समझ थी; उनकी क्या थी, नहीं मालूम !
लेकिन ऐसा बेजान और बेस्वाद गद्य किस काम का ? जिसमें न आकर्षण हो न लज़्ज़त ?
इसका भी उत्तर मुझे उन्हीं की बातों में मिला जो करते रहते थे। अक्सर ! भारतेन्दु युगीन गद्य के सन्दर्भ में। गुलेरी जी के सन्दर्भ में। कि संस्कृत और पुरानी हिन्दी का इतना बड़ा आचार्य लेकिन ‘उसने कहा था’ और ‘कछुआ-धर्म’ की भाषा देखो उनकी। तो ‘हँसमुख-गद्य’ आत्मीयता, जिन्दादिली और मस्ती से सराबोर हँसमुख गद्य ! बनारस की मिट्टी और आबोहवा में ही कुछ ऐसा है—फक्कड़ी, अक्खड़ी, हँसी-ठिठोली, व्यंग्य-विनोद, मौज-मस्ती। लेकिन इस किस्म का गद्य किसी टकसाल में नहीं, सड़कों पर, फुटपाथों पर, पंसारी और पनवाड़ी की दुकानों पर, रिक्शों-ठेलों पर मिलता है। इफारत भरा पड़ा है। जरूरत है उसे जीने की, साधने की। आलोचना की तो सीमाएँ हैं लेकिन रचनात्मक साहित्य की कोई सीमा नहीं।
अकादमिक तंत्र के भीतर कुलीनों के बीच रहनेवाले लेखक के लिए मुश्किल काम, लेकिन एक झरोखा तो खुला ही था मेरी आँखों के आगे।
उसे झरोखे से जो पहला चेहरा नजर आया, वह मेरे ही बड़े भाई का था !
यह कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि वे मेरे बड़े भाई ही नहीं, कथागुरु भी हैं। मुझमें जो भी थोड़ा-बहुत कथा-विवेक है, उन्हीं से अर्जित है। अगर मैं कहानी से संस्मरण की तरफ गया और फिर संस्मरण से कथा-रिपोर्ताज की ओर—तो इसके पीछे कहीं न कहीं वे भी हैं। उनके सिवा और कौन समझ सकता है कि मेरे कथकार की कमजोरियों और उसकी रचनात्मक ताकत को ? लम्बे-चौड़े मैदान में एक ही स्थान पर खड़े रहकर जिन्दगी भर ‘बाएँ-दाएँ’ करते रहने से बेहतर है अपनी सम्भावनाओं और क्षमताओं के लिए नए क्षितिज खोजना और किसी ऊसर पड़े खेत को हरा-भरा बनाना !
मैं उन्हें अपने कानों से पढ़ता रहा हूँ पिछले पचास वर्षों से। वे जो कहते रहते हैं, उसे कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते। ऐसा भी हुआ है कि जिस बात को सन् ’60 से कहते रहे हों, उसे 90 में जाकर लिखा हो। मैं जिस नगर में रहता हूँ वह मूल रूप से स्मृति और श्रुतिपरम्परा का ही नगर है। मुझे कहने में संकोच नहीं कि मैंने उन्हें कम से कम पढ़ा है और समझा तो उससे भी कम। लेकिन उनसे जो सुनता हूँ उनमें से अपने काम की या जरूरत की बातें गिरह बाँध लेता हूँ।
मुझे अपना पहला संस्मरण लिखना पड़ा उनकी ‘षष्टिपूर्ति पर ! ‘पहल’ के लिए ! यानी ’85-’86 के करीब ! कहानियाँ लिखते-लिखते ऊब-सा रहा था। कहानी से जो चाहता था, वह नहीं हो रहा था मुझसे। और संस्मरण के लिए हिन्दी में कोई मॉडल नहीं था मेरे सामने ! जो था वह रूखा, सूखा बेजान, अनाकर्षक, मांस-मज्जा हीन, ऊष्मा रहित। हड्डियों के निर्जीव ढाँचे की तरह। साथ ही संस्मरण की जगह साहित्य के समाज में उस दलित जैसी थी जिसके लिए ‘पंगत’ में कोई पत्तल नहीं।
मेरा कथाकार संस्मरण के शास्त्र को बदल देना चाहता था लेकिन यह उस पर नहीं, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के जीवन पर निर्भर था जो जीने की निर्धारित शास्त्रीयता को अस्वीकार कर रहे थे !
मुझे याद आया भैया का एक पत्र। सन् ’65 में बनारस छोड़ने के बाद का पहला पत्र। दिल्ली से। मुक्तिबोध को गुजरे कुछ ही महीने हो रहे थे और उन पर ‘राष्ट्रवाणी’ का एक अंक आया था। पत्र के अन्त में उन्होंने दो वाक्य लिखे थे-‘तुमने ‘राष्ट्रवाणी’ के मुक्तिबोध विशेषांक में छोटे भाई शरत मुक्तिबोध का निबंध पढ़ा ? पढ़ लेना, कौन जाने कभी तुम्हें भी लिखना पड़े तब याद रखना कि गद्य ऐसा ही हो-बल्कि इससे भी ज़्यादा खुश्क ! मैंने वह संस्मरण पढ़ा था लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं लगा था। इस चिट्ठी में मेरे मतलब की सिर्फ एक चीज़ थी कि गद्य कैसा हो ? खुश्क यानी गीला न हो, भीगा न हो-कपड़े उसे निचोड़ कर, पानी निथार कर सुखा लो और जब हल्का, कड़कड़ हो जाए, उसमें चमक आ जाए तब इस्तेमाल करो। राग-विराग मुक्त गद्य ! यह मेरी समझ थी; उनकी क्या थी, नहीं मालूम !
लेकिन ऐसा बेजान और बेस्वाद गद्य किस काम का ? जिसमें न आकर्षण हो न लज़्ज़त ?
इसका भी उत्तर मुझे उन्हीं की बातों में मिला जो करते रहते थे। अक्सर ! भारतेन्दु युगीन गद्य के सन्दर्भ में। गुलेरी जी के सन्दर्भ में। कि संस्कृत और पुरानी हिन्दी का इतना बड़ा आचार्य लेकिन ‘उसने कहा था’ और ‘कछुआ-धर्म’ की भाषा देखो उनकी। तो ‘हँसमुख-गद्य’ आत्मीयता, जिन्दादिली और मस्ती से सराबोर हँसमुख गद्य ! बनारस की मिट्टी और आबोहवा में ही कुछ ऐसा है—फक्कड़ी, अक्खड़ी, हँसी-ठिठोली, व्यंग्य-विनोद, मौज-मस्ती। लेकिन इस किस्म का गद्य किसी टकसाल में नहीं, सड़कों पर, फुटपाथों पर, पंसारी और पनवाड़ी की दुकानों पर, रिक्शों-ठेलों पर मिलता है। इफारत भरा पड़ा है। जरूरत है उसे जीने की, साधने की। आलोचना की तो सीमाएँ हैं लेकिन रचनात्मक साहित्य की कोई सीमा नहीं।
अकादमिक तंत्र के भीतर कुलीनों के बीच रहनेवाले लेखक के लिए मुश्किल काम, लेकिन एक झरोखा तो खुला ही था मेरी आँखों के आगे।
उसे झरोखे से जो पहला चेहरा नजर आया, वह मेरे ही बड़े भाई का था !
काशीनाथ
जीयनपुर
नामवर के गुरु हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कबीर के प्रसंग में लिखा था कि प्रतिभा जन्म लेने के लिए किसी कुल विशेष का इन्तज़ार नहीं करती। वे यह कहना भूल गए कि वह कभी-कभी इन्तज़ार भी करती है लेकिन टीले या ऊसर का—वरना नामवर को पैदा होने के लिए बनारस जिले में एक जीयनपुर ही नहीं था।
जीयनपुर को ऊसर गाँव बोलते थे उस जमाने में।
इस गाँव को पास-पड़ोस के धोबी जानते थे जिन्हें रेह की जरूरत पड़ती थी कपड़े धोने के लिए ! गिद्ध भी जानते थे। दैव भी जानता था। लेकिन जाने क्या था कि जब आस-पास के सारे गाँव पानी में डूबकर ‘त्राहि-त्राहि’ कर रहे होते थे, यह गाँव प्यासा का प्यासा रह जाता था।
नाम जीयनपुर और जीवन का पता नहीं !
हो सकता है, जीवन की चाहत ने ही इसे जीयनपुर नाम दिया हो।
लेकिन यह ‘पुर’ नहीं, ‘पुरवा’ था-किसी गाँव का पूरक। नामालूम-सी एक छोटी बस्ती !
बचपन में जैसे ही इस गाँव से बाहर निकलने लायक होने लगते थे, घर में पहला पाठ यही पढ़ाया जाता था कि अगर कहीं भटक गए या गुम हो गए, और कोई पूछे कहाँ घर है ? कहाँ रहते हो ? तो क्या बोलोगे ? और उत्तर रटाया जाता था-‘आवाजापुर ! जीयनपुर कहोगे तो कोई नहीं समझेगा !’
आवाजापुर रोड के किनारे। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा गाँव, ठाकुरों के कई टोले। कोई ऐसी जाति नहीं जो न हो। स्कूल भी, दवाखाना भी। ऐसा गाँव जिसमें सम्पन्न भी थे, शिक्षित भी, बाहर नौकरी करने वाले भी।
नामवर ने इसी गाँव में हिन्दी की वर्णमाला सीखी थी-‘न’ पर ‘आ’ की मात्रा ‘ना।’ जीयनपुर इसी आवाजपुर से एक मील पूरब था !
आइए, चलिए नामवर के बचपन के गाँव।
उत्तर तरफ गाँव की पूरी बस्ती को नापती हुई पोखर, जिसे ‘महदेवा’ बोलते थे— इसलिए कि पोखर के पार महादेव की पिंडी थी। शायद यह पोखर इसलिए थी कि इसी जगह की माटी से गाँव के घर दुआर बनाए जाते थे। पोखर पूरे गाँव की थी, किसी एक की नहीं।
गाँव के पूरब भीटा था-उत्तर से दक्खिन तक फैला हुआ जिस पर एक कतार में ताड़ के पेड़ थे-इसीलिए उसे कुछ लोग ताड़गाँव भी बोलते थे। ताड़ों पर गिद्धों और चीलों का बसेरा था ! उसी पर बैठकर वे सिवान में फेंके हुए या मरे हुए डाँगरों का जायजा लेते थे। रास्तों में अक्सर उनके उड़ने और पत्तों के खड़खड़ाने की आवाजें आती थीं। और जाड़ों में भोर के समय ताड़ों के बड़े-बड़े पके फूल भद्भद् गिरते तो हम उठकर नींद में दौड़ते और उठा लाते। उनके लिए लूट मची रहती थी।
कालू गोंड़ तो ताड़े भर उन्हीं के घात में रहते और उन्हीं पर गुजारा करते।
इन्हीं ताड़ों के बीच में नीम का एक बहुत बड़ा और गझिन पेड़ था जिस पर पचैंया (नागपंचमी) की शाम झूला पड़ता था। घराने के सभी मर्द-औरतें इस पर झूलते और कजली गाते थे। ‘हरी-हरी’ या ‘हरे रामा’ से शुरू होनेवाली कजलियाँ—आज भी कहीं झूला दिखाई पड़ता है, तो कानों में गूँजने लगती हैं। लड़के दिन में या शाम को झूलते थे और सयानी लड़कियाँ, बहुएँ या भाभियाँ रात या भोर में !
इसी नीम के नीचे अखाड़ा भी था।
ये ताड़ जहाँ खत्म होते थे-वहीं से पूरब के लिए छौरा जाता था जिसके मोड़ के पास काली माई का चौरा था। साल में दो बार गाँव की औरतें माता माई की पूजा करती थीं और चढ़ावे चढ़ाती थीं।
दक्खिनी सीमा पर बावड़ी थी जो भैसों के मड़िया लेने के काम आती थी ! फिर उसके बाद पठार जैसा भीटा जो गाँव और चमटोल के बीच ‘डिवाइडर’ था। इस भीटा पर पीपल का एक अकेला पुराना दरख्त था जिसके नीचे बरम बाबा !
चमटोल गाँव के दक्खिन थी-भीटा से परे !
हमारे हाईस्कूल की छमाही परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्र में एक सवाल पूछा गया था-‘चमटोल गाँव के दक्खिन ही क्यों होती है ?’ हम उत्तर नहीं दे सके थे लेकिन सचाई थी। उस पूरे इलाके में हर गाँव के
दक्खिन चमटोल। मास्टर ने बताया था कि चमारों की बस्तियाँ गन्दी, बदबूदार और रोगाणुओं से भरी होती हैं। हवाएँ प्रायः पूरब, पश्चिम और उत्तर से ही चलती हैं, दक्खिन से नहीं। इसलिए रोग व्याधि से गाँव की मुक्ति चमटोल के दक्खिन बसने में ही हैं ! देवी-देवताओं का वास भी उस दिशा में नहीं होता।
पच्छिम ऊसर था जिस पर डीह बाबा थे। गाँव के रक्षक ! सामान्य ज्ञान वाले प्रश्नपत्र में दूसरा प्रश्न भी यही था-‘डीह हमेशा गांव के पच्छिम ही क्यों होते हैं ?’ उत्तर भी उसी तरह के-कि गाँवों पर सारे आक्रमण पश्छिम से ही होते रहे हैं। सिकन्दर से लेकर मुगलों तक।
तो यह थी गाँव की चौगद्दी।
फसलें दो होती थीं-अगहनी और चेती ! जब तक धान नहीं तैयार होते तब तक गाँव बाजरा, जोन्हरी और सावाँ से काम चलाता। उन्हीं के दाने और उन्हीं के भात। धान की दो ही किस्में होती थीं-सारो और सिलहट। इनके भात लाल रंग के होते। समय-समय पर बाजरे और अरहर की खुद्दियों की लिट्टियाँ भी बनती रहतीं। जाड़ों की रात में भात और दिन में मटर की घुघनी और ईख का रस ! सब्जी मौसमी थीं। बरसात में करेम और सनई के फूलों के साग और जाड़ों में बथुआ और चने के !
गरमी की भोर की शुरुआत होती सिवान में महुवा बीनने से। दोपहर आम और जामुन के पीछे बगीचे में। रात को जौ की रोटियाँ बनतीं और अरहर की पनियल दाल। गेहूँ को ‘ब्राह्मण देवता’ कहा जाता था। थोड़ा बहुत होता भी तो शादी-ब्याह और श्राद्ध के लिए रखा रहता। प्रायः हर घर में एक-एक भैंस थी लेकिन जब ब्यासी होती तो उसका मट्ठा ही मिलता-वह भी नपने से, उम्र के हिसाब से ! दूध या दही के दर्शन खिचड़ी (मकर संक्राति) को होते, चिउड़ा के साथ।
यह सारा कुछ इसलिए कि सिंचाई कुएँ या दैव के भरोसे थी।
कहते हैं, कोई घूरी सिंह थे खड़ान गाँव में-उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ! महारानी विक्टोरिया के राज में हिन्दुस्तानी फौज में सूबेदार ! लम्बे तगड़े मजबूत कद-काठी के जवान। बहादुर और दिलेर। अपने रेजिमेंट के साथ कहीं उत्तर-पूरब में पड़े हुए थे ! जंगली पहाड़ी घनघोर इलाका। जाड़े के दिन थे। सुबह शौच के लिए लोटे में पानी लेकर निकले और दूर चले गए छावनी से ! वे बैठे ही थे निपटने के लिए कि एक बाघ ने उन पर आक्रमण कर दिया। उस बाघ ने आतंक मचा रखा था उस इलाके में। वे सुन चुके थे उसके बारे में। चालाक से चालाक शिकारी भी उससे हार मार चुके थे। घूरी के पास कोई हथियार नहीं था सिवा कम्बल और लौटे के ! वे उस पर कम्बल फेंक कर टूट पड़े। किसी तरह गरदन समेत जबड़े को कम्बल में लपेटा और लोटे से ताबड़तोड़ शुरू किया माथे पर। वे लहूलुहान हो गए लेकिन मारते रहे ! धीरे-धीरे वह घुर्रघुर्र करने के बाद ठंडा हो गया।
खबर पहुँची बर्तानिया सरकार के आला अफसरों के पास। उन्होंने जब बाघ की खाल, चिथड़ा कम्बल और पिचका लोटा देखा तो विश्वास हो गया। उन्हीं की सिफारिश पर इनाम में घूरी को तीन गाँव दिए गए-पहाड़पुर, करजौंड़ा और जीयनपुर। खड़ान गाँव इन गाँवों से तीन-चार मील दूर ! कैसे सम्भव थी इनकी देख भाल ? करजौंड़ा और पहाड़पुर में पहले से बसाहट थी, बस्तियाँ थीं, लोग थे। इस हिसाब से जीयनपुर ठीक लगा उन्हें। यहाँ सिर्फ ठाकुरों के दो घर थे-बाकी नागफनी के जंगल, झाड-झंखाड़ ऊसर और रेह। न कहीं तालाब, न पोखर, न नदी-नाला। खुला मैदान और खुली छूट ! जीयनपुर से करजौड़ा और पहाड़पुर की भी देखरेख की जा सकती थी।
मौजूदा जीयनपुर इन्हीं तीनों परिवारों का विस्तार है।
घूरी के चार बेटे हुए-अयोध्या, मथुरा, द्वारिका और हरगेन। फिर इन सबकी सन्तानें हुईं। द्वारिका के भी चार बेटे हुए-मकुनी, गोकुल, रामजग, और रामनाथ। इनमें जब बँटवारा हुआ तो रामनाथ के हिस्से तीस बीघे खेत आए। रामनाथ को खेतों से नहीं, सिर्फ भैंस से मतलब था ! सीधे सीदे। अँगूठा टेक साधु स्वभाव के आदमी। घर-दुआर जगह-जायदाद किस काम के ? सुबह-सुबह वे खूँटे से भैंस खोलते और सिवान में निकल जाते ! उनका सारा समय सिवान बाग-बगीचों और ताल-तलैयों में ही गुजरता ! इस तरह भैंस की सेवा करते-करते एक दिन वे अपनी जवानी में ही सुरलोक सिधार गए।
रह गए उनके बेटे-सागर, नागर, बाबूनन्दन और जयराम ! बचपन में ही जयरान के गुजरने के बावजूद ठाकुरों में सबसे बड़ा परिवार। छोटे-बड़े मिलाकर लगभग बीस सदस्य ! सिर्फ बड़ा, नहीं, सम्मानित भी। पूरे गाँव में यही एक घर था जिसमें खेती बाड़ी के सिवा बाहर से भी हर महीने सोलह रुपए की आय थी। और यह आय थी प्राइमरी स्कूल के मास्टर की।
इन्हीं मास्टर का नाम नागर सिंह था और इन्हीं के बड़े बेटे हैं नामवर !
मास्टर तो दूसरे गाँवों में भी थे-प्राइमरी के ही नहीं मिडलस्कूल तक के लेकिन इनकी कुछ अपनी ख़ासियत थी। ये कभी गाँव के पचड़ों झगड़ों में पड़े नहीं-अपने घरानों या पट्टीदार के हों या छोटी-बड़ी जातियों के ! अपने काम से काम। न किसी की चुगली सुनना और न खाना। नाच तमाशे और हा-हा हू-बू से कोई मतलब नहीं। बच्चे चाहे जिस जाति के हों-उन्हें डाँट-डपट के स्कूल भिजवाते रहते थे। पाखंड, धूर्तता और झूठ से चिढ़ थी उन्हें। हुक्का पीते थे-घर पर भी और स्कूल में भी। हमेशा छड़ी या छाता लिए हुए चलते थे-नाक की सीध में; और सिर्फ चलते नहीं थे, देखते भी थे। बेहद नियमित और अनुशासित ! कभी नहीं पाया कि स्कूल खुला हो और वे घर के काम निपटाने में लगे हों। गिरस्ती का काम न वे करते थे और न कोई करने के लिए उनसे कहता था।
लोग उनसे डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे।
‘मास्टर’ के एक मित्र थे विद्यार्थी जी। गाँधीवादी और सुराजी ! बाद में विधायक हुए कांग्रेस से ! उन दिनों एक-डेढ़ मील पूरब रहते थे हेतमपुर में। छुट्टियों में तो वहाँ जाने का नियम सा बना रखा था। शायद उन्हीं की देखा-देखी मारकीन छोड़कर खद्दर पहनना शुरू कर दिया था उन्होंने और नौकरी छोड़ने का मन भी बना लिया था।
जीयनपुर में शिक्षा इन्हीं मास्टर के जरिए आई थी !
मास्टर के बड़े भाई थे सागर सिंह सामाजिक, व्यवहार कुशल और हँसमुख। वही घर के मालिक थे ! छोटे भाई बाबूनन्दन गाने-बजाने वाले घुमन्तू और बैठकबाज थे। तीन भाई तीन रकम के थे। लेकिन ये तीनों भाई एक-दूसरे की बड़ी इज़्ज़त करते थे। बथरी में होनेवाली औरतों की काँव-काँव-झाँव-झाँव से वे अप्रभावित रहते थे। उनकी मान्यता थी कि हम एक खून और एक संस्कार के हैं लेकिन ये औरतें अलग-अलग घरों से आई हैं, इनके संस्कार अलग-अलग हैं; कि ये मिट्टी के सात घड़े हैं, पास-पास रहेंगे तो टकराएँगे ही, टकराएँगे तो आवाज होगी ही। इन पर कान देने की कोई जरूरत नहीं। उनकी यह समझ उनके व्यवहार में भी दिखाई पड़ती। वे अपने नहीं, दूसरे के बेटो को अपना बेटा मानते।
लेकिन औरतों में यह समझदारी नहीं थी। उनके बेटे ही उनके लिए सब कुछ थे। वे आपस में लड़ते तो उनकी माँएँ लड़ पड़तीं। बेटों के पीछे उनके गुट बनते बिगड़ते रहते ! और उसी के भरोसे वे अपने बच्चों के खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने की अलग से व्यवस्था भी रखती थीं-निजी।
माँ की स्थिति थोड़ी अलग थी, इन औरतों के मुकाबले ! उसका मायका नहीं रह गया था। शादी के बाद ही वहाँ महामारी फैली थी और सारा कुछ खत्म हो गया था। उसकी माँ की बहन का घर ही उसका मायका था जहाँ वह कभी नहीं गई ! दूसरी मुश्किल यह थी कि सबके पति हमेशा खेत-खलिहान में लगे रहते लेकिन उसके पति को मुदर्रिसी से ही फुर्सत न थी। जब कभी मिलती भी थी तो उनकी दिलचस्पी ही न थी ! दुआर पर लेटे-लेटे टाँगें हिलाया करते। जबकि खाने में न वे कोई कसर छोड़ते, न उनके बेटे ! उन्हें तो कोई कुछ न बोलता लेकिन औरतें सारा गुस्सा माँ पर निकालती रहतीं।
सबसे बड़ी बात यह कि उसने अपने पति की कमाई का सुख भी कभी नहीं जाना। क्योंकि उनकी कमाई एक सरकारी खजाने से निकलती और परिवार के सरकारी खजाने में चली जाती।
एक दुख बराबर सालता रहा उसे पति पढ़ा-लिखा और वह अपढ़ गँवार। वह अक्सर कहा करती कि अगर उसके गाँव में स्कूल रहा होता तो जरूर पढ़ा होता। पढ़ने का सुख उसने तब जाना जब उसके बड़े बेटे को वजीफा मिला। उसी के पैसों में उसने बकरी खरीदी अपने बच्चों के दूध पीने के लिए। वह चाहती थी कि उसके बेटे खूब पढें-बड़ा आदमी बनें। लेकिन किसान का घर। काम ही काम। कटाई है, जुताई, हेंगाई है, दँवाई है, रोपनी है, बुवाई है, ईख छोलाई है, कोल्हुआड़ है, मोट-पुर है, दारी है, बिनिया है, खेतवाही है और नहीं तो दिन चढ़ आया है और भैंस अभी खूँटे पर ही है-काम से जी न चुराना हो तो काम ही काम है। उसे लगता कि सबको काम तभी सूझता है जब उसका बेटा पढ़ने बैठता है ! और दूसरों को लगता कि दूसरे लड़के बच्चे सुबह से खट रहे हैं और यह ससुर कापी गोंद रहे हैं। अरे, जो जरूरी है पहले वह देखो, किताब कहीं भागे थोड़े जा रही है ? बीच में माँ के बोलने का मतलब होता- झगड़ा।
माँ इकहरे बदन की लम्बी, गोरी खूबसूरत और धर्मभीरू औरत थी-छोटी से छोटी बात पर मनौती मानने वाली ! खुशदिल और हँसमुख। गाने बजाने के हर त्यौहार और मौके पर हाज़िर। किसी की भी अर्थी जाते देखकर रोना और किसी भी आँगन में विवाह का माँड़ो गड़ा देखकर गाना उसका स्वभाव था। रोना इस बात पर कि अब क्या होगा उस विधवा का ? या माँ का ? या खानदान का ? गाना इस बात पर कि कितनी खुश होगी बेटी ? उसके माँ-बाप ? उसके घर वाले ? उसे जब-जब ये याद आते गाती या रोती ! जिन्होंने उसे देखा था और बातें की थीं वे नामवर के नामवर होने का श्रेय माँ को देते हैं। उसने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए अपना गहना-गुरिया सारा कुछ बेच डाला था।
अपने बेटे को लेकर पिता के सपने बड़े छोटे थे। उनके सपनों की ऊँचाई जीयनपुर के टीलों से अधिक न थी। इससे अधिक के बारे में सोच भी नहीं सकते थे वे ! वे चाहते थे कि बड़के जने (जीवन भर उनके मुँह से यही सुना कभी नामवर नहीं) मिडल पास करने के बाद नार्मल की ट्रेनिंग करें और गाँव के आस-पास किसी स्कूल में मास्टर हो जाएँ। खेती बारी भी सँभालें और पढ़ाएँ भी।
यह नामवर को स्वीकर न हुआ और इस मामले में माँ बेटे के साथ थी।
मित्रों, इस लम्बी-लम्बी भूमिका के बाद मैं आपको सच्ची बात यह बताऊँ कि मैंने नामवर के बचपन का गाँव जरूर देखा है, उनका बचपन नहीं देखा। वे मुझसे दस साल बड़े थे। वे सन् 41 में जीयनपुर छोड़ गए जब मैं चार-पाँच साल का था ! बड़े भाई के नाम पर मैं सिर्फ़ रामजी को जानता था। माँ बताती रही होगी लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं।
धीरे-धीरे सुनना शुरू किया उनके बारे में-
कि पढ़ने में बड़े तेज थे,
कि इतिहास के पर्चे में किसी एक ही प्रश्न का उत्तर लिखते रहे थे, इसलिए मिडल में फेल हो गए।
कि कादिराबाद में कोई वाचनालय या लाइब्रेरी थी जहाँ अक्सर जाते थे।
जीयनपुर को ऊसर गाँव बोलते थे उस जमाने में।
इस गाँव को पास-पड़ोस के धोबी जानते थे जिन्हें रेह की जरूरत पड़ती थी कपड़े धोने के लिए ! गिद्ध भी जानते थे। दैव भी जानता था। लेकिन जाने क्या था कि जब आस-पास के सारे गाँव पानी में डूबकर ‘त्राहि-त्राहि’ कर रहे होते थे, यह गाँव प्यासा का प्यासा रह जाता था।
नाम जीयनपुर और जीवन का पता नहीं !
हो सकता है, जीवन की चाहत ने ही इसे जीयनपुर नाम दिया हो।
लेकिन यह ‘पुर’ नहीं, ‘पुरवा’ था-किसी गाँव का पूरक। नामालूम-सी एक छोटी बस्ती !
बचपन में जैसे ही इस गाँव से बाहर निकलने लायक होने लगते थे, घर में पहला पाठ यही पढ़ाया जाता था कि अगर कहीं भटक गए या गुम हो गए, और कोई पूछे कहाँ घर है ? कहाँ रहते हो ? तो क्या बोलोगे ? और उत्तर रटाया जाता था-‘आवाजापुर ! जीयनपुर कहोगे तो कोई नहीं समझेगा !’
आवाजापुर रोड के किनारे। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा गाँव, ठाकुरों के कई टोले। कोई ऐसी जाति नहीं जो न हो। स्कूल भी, दवाखाना भी। ऐसा गाँव जिसमें सम्पन्न भी थे, शिक्षित भी, बाहर नौकरी करने वाले भी।
नामवर ने इसी गाँव में हिन्दी की वर्णमाला सीखी थी-‘न’ पर ‘आ’ की मात्रा ‘ना।’ जीयनपुर इसी आवाजपुर से एक मील पूरब था !
आइए, चलिए नामवर के बचपन के गाँव।
उत्तर तरफ गाँव की पूरी बस्ती को नापती हुई पोखर, जिसे ‘महदेवा’ बोलते थे— इसलिए कि पोखर के पार महादेव की पिंडी थी। शायद यह पोखर इसलिए थी कि इसी जगह की माटी से गाँव के घर दुआर बनाए जाते थे। पोखर पूरे गाँव की थी, किसी एक की नहीं।
गाँव के पूरब भीटा था-उत्तर से दक्खिन तक फैला हुआ जिस पर एक कतार में ताड़ के पेड़ थे-इसीलिए उसे कुछ लोग ताड़गाँव भी बोलते थे। ताड़ों पर गिद्धों और चीलों का बसेरा था ! उसी पर बैठकर वे सिवान में फेंके हुए या मरे हुए डाँगरों का जायजा लेते थे। रास्तों में अक्सर उनके उड़ने और पत्तों के खड़खड़ाने की आवाजें आती थीं। और जाड़ों में भोर के समय ताड़ों के बड़े-बड़े पके फूल भद्भद् गिरते तो हम उठकर नींद में दौड़ते और उठा लाते। उनके लिए लूट मची रहती थी।
कालू गोंड़ तो ताड़े भर उन्हीं के घात में रहते और उन्हीं पर गुजारा करते।
इन्हीं ताड़ों के बीच में नीम का एक बहुत बड़ा और गझिन पेड़ था जिस पर पचैंया (नागपंचमी) की शाम झूला पड़ता था। घराने के सभी मर्द-औरतें इस पर झूलते और कजली गाते थे। ‘हरी-हरी’ या ‘हरे रामा’ से शुरू होनेवाली कजलियाँ—आज भी कहीं झूला दिखाई पड़ता है, तो कानों में गूँजने लगती हैं। लड़के दिन में या शाम को झूलते थे और सयानी लड़कियाँ, बहुएँ या भाभियाँ रात या भोर में !
इसी नीम के नीचे अखाड़ा भी था।
ये ताड़ जहाँ खत्म होते थे-वहीं से पूरब के लिए छौरा जाता था जिसके मोड़ के पास काली माई का चौरा था। साल में दो बार गाँव की औरतें माता माई की पूजा करती थीं और चढ़ावे चढ़ाती थीं।
दक्खिनी सीमा पर बावड़ी थी जो भैसों के मड़िया लेने के काम आती थी ! फिर उसके बाद पठार जैसा भीटा जो गाँव और चमटोल के बीच ‘डिवाइडर’ था। इस भीटा पर पीपल का एक अकेला पुराना दरख्त था जिसके नीचे बरम बाबा !
चमटोल गाँव के दक्खिन थी-भीटा से परे !
हमारे हाईस्कूल की छमाही परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्र में एक सवाल पूछा गया था-‘चमटोल गाँव के दक्खिन ही क्यों होती है ?’ हम उत्तर नहीं दे सके थे लेकिन सचाई थी। उस पूरे इलाके में हर गाँव के
दक्खिन चमटोल। मास्टर ने बताया था कि चमारों की बस्तियाँ गन्दी, बदबूदार और रोगाणुओं से भरी होती हैं। हवाएँ प्रायः पूरब, पश्चिम और उत्तर से ही चलती हैं, दक्खिन से नहीं। इसलिए रोग व्याधि से गाँव की मुक्ति चमटोल के दक्खिन बसने में ही हैं ! देवी-देवताओं का वास भी उस दिशा में नहीं होता।
पच्छिम ऊसर था जिस पर डीह बाबा थे। गाँव के रक्षक ! सामान्य ज्ञान वाले प्रश्नपत्र में दूसरा प्रश्न भी यही था-‘डीह हमेशा गांव के पच्छिम ही क्यों होते हैं ?’ उत्तर भी उसी तरह के-कि गाँवों पर सारे आक्रमण पश्छिम से ही होते रहे हैं। सिकन्दर से लेकर मुगलों तक।
तो यह थी गाँव की चौगद्दी।
फसलें दो होती थीं-अगहनी और चेती ! जब तक धान नहीं तैयार होते तब तक गाँव बाजरा, जोन्हरी और सावाँ से काम चलाता। उन्हीं के दाने और उन्हीं के भात। धान की दो ही किस्में होती थीं-सारो और सिलहट। इनके भात लाल रंग के होते। समय-समय पर बाजरे और अरहर की खुद्दियों की लिट्टियाँ भी बनती रहतीं। जाड़ों की रात में भात और दिन में मटर की घुघनी और ईख का रस ! सब्जी मौसमी थीं। बरसात में करेम और सनई के फूलों के साग और जाड़ों में बथुआ और चने के !
गरमी की भोर की शुरुआत होती सिवान में महुवा बीनने से। दोपहर आम और जामुन के पीछे बगीचे में। रात को जौ की रोटियाँ बनतीं और अरहर की पनियल दाल। गेहूँ को ‘ब्राह्मण देवता’ कहा जाता था। थोड़ा बहुत होता भी तो शादी-ब्याह और श्राद्ध के लिए रखा रहता। प्रायः हर घर में एक-एक भैंस थी लेकिन जब ब्यासी होती तो उसका मट्ठा ही मिलता-वह भी नपने से, उम्र के हिसाब से ! दूध या दही के दर्शन खिचड़ी (मकर संक्राति) को होते, चिउड़ा के साथ।
यह सारा कुछ इसलिए कि सिंचाई कुएँ या दैव के भरोसे थी।
कहते हैं, कोई घूरी सिंह थे खड़ान गाँव में-उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ! महारानी विक्टोरिया के राज में हिन्दुस्तानी फौज में सूबेदार ! लम्बे तगड़े मजबूत कद-काठी के जवान। बहादुर और दिलेर। अपने रेजिमेंट के साथ कहीं उत्तर-पूरब में पड़े हुए थे ! जंगली पहाड़ी घनघोर इलाका। जाड़े के दिन थे। सुबह शौच के लिए लोटे में पानी लेकर निकले और दूर चले गए छावनी से ! वे बैठे ही थे निपटने के लिए कि एक बाघ ने उन पर आक्रमण कर दिया। उस बाघ ने आतंक मचा रखा था उस इलाके में। वे सुन चुके थे उसके बारे में। चालाक से चालाक शिकारी भी उससे हार मार चुके थे। घूरी के पास कोई हथियार नहीं था सिवा कम्बल और लौटे के ! वे उस पर कम्बल फेंक कर टूट पड़े। किसी तरह गरदन समेत जबड़े को कम्बल में लपेटा और लोटे से ताबड़तोड़ शुरू किया माथे पर। वे लहूलुहान हो गए लेकिन मारते रहे ! धीरे-धीरे वह घुर्रघुर्र करने के बाद ठंडा हो गया।
खबर पहुँची बर्तानिया सरकार के आला अफसरों के पास। उन्होंने जब बाघ की खाल, चिथड़ा कम्बल और पिचका लोटा देखा तो विश्वास हो गया। उन्हीं की सिफारिश पर इनाम में घूरी को तीन गाँव दिए गए-पहाड़पुर, करजौंड़ा और जीयनपुर। खड़ान गाँव इन गाँवों से तीन-चार मील दूर ! कैसे सम्भव थी इनकी देख भाल ? करजौंड़ा और पहाड़पुर में पहले से बसाहट थी, बस्तियाँ थीं, लोग थे। इस हिसाब से जीयनपुर ठीक लगा उन्हें। यहाँ सिर्फ ठाकुरों के दो घर थे-बाकी नागफनी के जंगल, झाड-झंखाड़ ऊसर और रेह। न कहीं तालाब, न पोखर, न नदी-नाला। खुला मैदान और खुली छूट ! जीयनपुर से करजौड़ा और पहाड़पुर की भी देखरेख की जा सकती थी।
मौजूदा जीयनपुर इन्हीं तीनों परिवारों का विस्तार है।
घूरी के चार बेटे हुए-अयोध्या, मथुरा, द्वारिका और हरगेन। फिर इन सबकी सन्तानें हुईं। द्वारिका के भी चार बेटे हुए-मकुनी, गोकुल, रामजग, और रामनाथ। इनमें जब बँटवारा हुआ तो रामनाथ के हिस्से तीस बीघे खेत आए। रामनाथ को खेतों से नहीं, सिर्फ भैंस से मतलब था ! सीधे सीदे। अँगूठा टेक साधु स्वभाव के आदमी। घर-दुआर जगह-जायदाद किस काम के ? सुबह-सुबह वे खूँटे से भैंस खोलते और सिवान में निकल जाते ! उनका सारा समय सिवान बाग-बगीचों और ताल-तलैयों में ही गुजरता ! इस तरह भैंस की सेवा करते-करते एक दिन वे अपनी जवानी में ही सुरलोक सिधार गए।
रह गए उनके बेटे-सागर, नागर, बाबूनन्दन और जयराम ! बचपन में ही जयरान के गुजरने के बावजूद ठाकुरों में सबसे बड़ा परिवार। छोटे-बड़े मिलाकर लगभग बीस सदस्य ! सिर्फ बड़ा, नहीं, सम्मानित भी। पूरे गाँव में यही एक घर था जिसमें खेती बाड़ी के सिवा बाहर से भी हर महीने सोलह रुपए की आय थी। और यह आय थी प्राइमरी स्कूल के मास्टर की।
इन्हीं मास्टर का नाम नागर सिंह था और इन्हीं के बड़े बेटे हैं नामवर !
मास्टर तो दूसरे गाँवों में भी थे-प्राइमरी के ही नहीं मिडलस्कूल तक के लेकिन इनकी कुछ अपनी ख़ासियत थी। ये कभी गाँव के पचड़ों झगड़ों में पड़े नहीं-अपने घरानों या पट्टीदार के हों या छोटी-बड़ी जातियों के ! अपने काम से काम। न किसी की चुगली सुनना और न खाना। नाच तमाशे और हा-हा हू-बू से कोई मतलब नहीं। बच्चे चाहे जिस जाति के हों-उन्हें डाँट-डपट के स्कूल भिजवाते रहते थे। पाखंड, धूर्तता और झूठ से चिढ़ थी उन्हें। हुक्का पीते थे-घर पर भी और स्कूल में भी। हमेशा छड़ी या छाता लिए हुए चलते थे-नाक की सीध में; और सिर्फ चलते नहीं थे, देखते भी थे। बेहद नियमित और अनुशासित ! कभी नहीं पाया कि स्कूल खुला हो और वे घर के काम निपटाने में लगे हों। गिरस्ती का काम न वे करते थे और न कोई करने के लिए उनसे कहता था।
लोग उनसे डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे।
‘मास्टर’ के एक मित्र थे विद्यार्थी जी। गाँधीवादी और सुराजी ! बाद में विधायक हुए कांग्रेस से ! उन दिनों एक-डेढ़ मील पूरब रहते थे हेतमपुर में। छुट्टियों में तो वहाँ जाने का नियम सा बना रखा था। शायद उन्हीं की देखा-देखी मारकीन छोड़कर खद्दर पहनना शुरू कर दिया था उन्होंने और नौकरी छोड़ने का मन भी बना लिया था।
जीयनपुर में शिक्षा इन्हीं मास्टर के जरिए आई थी !
मास्टर के बड़े भाई थे सागर सिंह सामाजिक, व्यवहार कुशल और हँसमुख। वही घर के मालिक थे ! छोटे भाई बाबूनन्दन गाने-बजाने वाले घुमन्तू और बैठकबाज थे। तीन भाई तीन रकम के थे। लेकिन ये तीनों भाई एक-दूसरे की बड़ी इज़्ज़त करते थे। बथरी में होनेवाली औरतों की काँव-काँव-झाँव-झाँव से वे अप्रभावित रहते थे। उनकी मान्यता थी कि हम एक खून और एक संस्कार के हैं लेकिन ये औरतें अलग-अलग घरों से आई हैं, इनके संस्कार अलग-अलग हैं; कि ये मिट्टी के सात घड़े हैं, पास-पास रहेंगे तो टकराएँगे ही, टकराएँगे तो आवाज होगी ही। इन पर कान देने की कोई जरूरत नहीं। उनकी यह समझ उनके व्यवहार में भी दिखाई पड़ती। वे अपने नहीं, दूसरे के बेटो को अपना बेटा मानते।
लेकिन औरतों में यह समझदारी नहीं थी। उनके बेटे ही उनके लिए सब कुछ थे। वे आपस में लड़ते तो उनकी माँएँ लड़ पड़तीं। बेटों के पीछे उनके गुट बनते बिगड़ते रहते ! और उसी के भरोसे वे अपने बच्चों के खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने की अलग से व्यवस्था भी रखती थीं-निजी।
माँ की स्थिति थोड़ी अलग थी, इन औरतों के मुकाबले ! उसका मायका नहीं रह गया था। शादी के बाद ही वहाँ महामारी फैली थी और सारा कुछ खत्म हो गया था। उसकी माँ की बहन का घर ही उसका मायका था जहाँ वह कभी नहीं गई ! दूसरी मुश्किल यह थी कि सबके पति हमेशा खेत-खलिहान में लगे रहते लेकिन उसके पति को मुदर्रिसी से ही फुर्सत न थी। जब कभी मिलती भी थी तो उनकी दिलचस्पी ही न थी ! दुआर पर लेटे-लेटे टाँगें हिलाया करते। जबकि खाने में न वे कोई कसर छोड़ते, न उनके बेटे ! उन्हें तो कोई कुछ न बोलता लेकिन औरतें सारा गुस्सा माँ पर निकालती रहतीं।
सबसे बड़ी बात यह कि उसने अपने पति की कमाई का सुख भी कभी नहीं जाना। क्योंकि उनकी कमाई एक सरकारी खजाने से निकलती और परिवार के सरकारी खजाने में चली जाती।
एक दुख बराबर सालता रहा उसे पति पढ़ा-लिखा और वह अपढ़ गँवार। वह अक्सर कहा करती कि अगर उसके गाँव में स्कूल रहा होता तो जरूर पढ़ा होता। पढ़ने का सुख उसने तब जाना जब उसके बड़े बेटे को वजीफा मिला। उसी के पैसों में उसने बकरी खरीदी अपने बच्चों के दूध पीने के लिए। वह चाहती थी कि उसके बेटे खूब पढें-बड़ा आदमी बनें। लेकिन किसान का घर। काम ही काम। कटाई है, जुताई, हेंगाई है, दँवाई है, रोपनी है, बुवाई है, ईख छोलाई है, कोल्हुआड़ है, मोट-पुर है, दारी है, बिनिया है, खेतवाही है और नहीं तो दिन चढ़ आया है और भैंस अभी खूँटे पर ही है-काम से जी न चुराना हो तो काम ही काम है। उसे लगता कि सबको काम तभी सूझता है जब उसका बेटा पढ़ने बैठता है ! और दूसरों को लगता कि दूसरे लड़के बच्चे सुबह से खट रहे हैं और यह ससुर कापी गोंद रहे हैं। अरे, जो जरूरी है पहले वह देखो, किताब कहीं भागे थोड़े जा रही है ? बीच में माँ के बोलने का मतलब होता- झगड़ा।
माँ इकहरे बदन की लम्बी, गोरी खूबसूरत और धर्मभीरू औरत थी-छोटी से छोटी बात पर मनौती मानने वाली ! खुशदिल और हँसमुख। गाने बजाने के हर त्यौहार और मौके पर हाज़िर। किसी की भी अर्थी जाते देखकर रोना और किसी भी आँगन में विवाह का माँड़ो गड़ा देखकर गाना उसका स्वभाव था। रोना इस बात पर कि अब क्या होगा उस विधवा का ? या माँ का ? या खानदान का ? गाना इस बात पर कि कितनी खुश होगी बेटी ? उसके माँ-बाप ? उसके घर वाले ? उसे जब-जब ये याद आते गाती या रोती ! जिन्होंने उसे देखा था और बातें की थीं वे नामवर के नामवर होने का श्रेय माँ को देते हैं। उसने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए अपना गहना-गुरिया सारा कुछ बेच डाला था।
अपने बेटे को लेकर पिता के सपने बड़े छोटे थे। उनके सपनों की ऊँचाई जीयनपुर के टीलों से अधिक न थी। इससे अधिक के बारे में सोच भी नहीं सकते थे वे ! वे चाहते थे कि बड़के जने (जीवन भर उनके मुँह से यही सुना कभी नामवर नहीं) मिडल पास करने के बाद नार्मल की ट्रेनिंग करें और गाँव के आस-पास किसी स्कूल में मास्टर हो जाएँ। खेती बारी भी सँभालें और पढ़ाएँ भी।
यह नामवर को स्वीकर न हुआ और इस मामले में माँ बेटे के साथ थी।
मित्रों, इस लम्बी-लम्बी भूमिका के बाद मैं आपको सच्ची बात यह बताऊँ कि मैंने नामवर के बचपन का गाँव जरूर देखा है, उनका बचपन नहीं देखा। वे मुझसे दस साल बड़े थे। वे सन् 41 में जीयनपुर छोड़ गए जब मैं चार-पाँच साल का था ! बड़े भाई के नाम पर मैं सिर्फ़ रामजी को जानता था। माँ बताती रही होगी लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं।
धीरे-धीरे सुनना शुरू किया उनके बारे में-
कि पढ़ने में बड़े तेज थे,
कि इतिहास के पर्चे में किसी एक ही प्रश्न का उत्तर लिखते रहे थे, इसलिए मिडल में फेल हो गए।
कि कादिराबाद में कोई वाचनालय या लाइब्रेरी थी जहाँ अक्सर जाते थे।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book