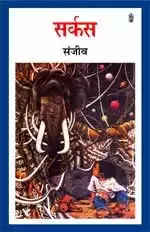|
विविध >> सर्कस सर्कससंजीव
|
325 पाठक हैं |
||||||
इसमें सर्कस के पहलुओं को दर्शाया गया है....
Sarkas
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
सर्कस आज एक खत्म होती हुई कला है। सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन के अभाव, आधुनिक टेक्नॉलॉजी-आधारित मनोरंजन के प्रभुत्व और उसकी अपनी आन्तरिक समस्याओं के चलते वह अपनी पारम्परिक जगह को खोता जा रहा है लेकिन आज भी वह न सिर्फ एक बड़े दर्शक वर्ग को आकर्षित करता है, बल्कि एक कौतूहल की रचना भी करता है।
उस विशाल तम्बू के भीतर जहाँ शो शुरू होते ही जैसे जिंदगी और खुशी नाचने लगती है, सुख, दुःख, आशा-निराशा, यातना और उत्पीड़न का एक भरा-पूरा संसार भी रहता है। खासतौर से भारतीय सर्कस अपने अभावों और भविष्यहीनता के चलते एक बहुस्तरीय यंत्रणा का परकोट है।
हमारे समय के वरिष्ठ कथाकार संजीव का यह उपन्यास उस दुनिया के भीतर उतरता है, और सर्कस के उन पहलुओं को हमें दिखाता है, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह चाहे वहाँ काम करने वाले लोगों की पीड़ा हो, या जानवरों की, हमें ऐसे अनुभव से रूबरू कराती है जो दर्शक के रूप में हमारे लिए अलभ्य रहे आये हैं।
सर्कस सिर्फ शामियाने के भीतर चलने वाला तमाशा ही नहीं, देश का विराट रूपक भी है जहाँ अभिनेता अपनी-अपनी आकांक्षाओं, द्वन्द्वों और छद्म में साँस लेते हुए दर्शक का मनोरंजन करते हैं।
उस विशाल तम्बू के भीतर जहाँ शो शुरू होते ही जैसे जिंदगी और खुशी नाचने लगती है, सुख, दुःख, आशा-निराशा, यातना और उत्पीड़न का एक भरा-पूरा संसार भी रहता है। खासतौर से भारतीय सर्कस अपने अभावों और भविष्यहीनता के चलते एक बहुस्तरीय यंत्रणा का परकोट है।
हमारे समय के वरिष्ठ कथाकार संजीव का यह उपन्यास उस दुनिया के भीतर उतरता है, और सर्कस के उन पहलुओं को हमें दिखाता है, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह चाहे वहाँ काम करने वाले लोगों की पीड़ा हो, या जानवरों की, हमें ऐसे अनुभव से रूबरू कराती है जो दर्शक के रूप में हमारे लिए अलभ्य रहे आये हैं।
सर्कस सिर्फ शामियाने के भीतर चलने वाला तमाशा ही नहीं, देश का विराट रूपक भी है जहाँ अभिनेता अपनी-अपनी आकांक्षाओं, द्वन्द्वों और छद्म में साँस लेते हुए दर्शक का मनोरंजन करते हैं।
देश के मेहनतकश अवाम के प्रतीक
पिताश्री की समृति में
जिन्हें गुमान होता है कि वे भी
‘सर्कस’ के कलाकार हैं,
मगर हकीकत यह खुलती है
कि वे महज दर्शक हैं।
अपनी बात
बीते हुए दिनों के ठहरे हुए अक्स। राख और मलबे के ढेर को आज खुरचने बैठा हूँ तो अबरख के चकत्तों के मनिन्द जाने कितने हारे हुए, जीते हुए, क्षण, कुम्हालाए, सड़े फूल और पत्ते, मध्याहृ के उतरे सूरज की रोशनी में चिलक उठे हैं। एक बार, दो बार जितनी बार हाथ फेरता हूँ बकरे के कटे मुंड में पथराई आँखों के कितने आयाम खिल-खिल उठते है- एक-दूजे में गुँथे-बिंधे!
जीवन के निबन्ध व्याकरण ने कितनी ही संज्ञाएँ दीं- संजीवन, संजीवन, सजेवन, साजन, सजावन और संजीव। इन तत्सम, तद्भव, देशज. विदेशज (?) नामों के साथ राम और प्रसाद के उपमार्ग-प्रत्यय और ‘मास्टर’ का सर्वनाम-विश्लेषण। जन्म की तिथि मेरे जैसे परिवार के लिए कोई महत्त्व की बात नहीं थी, अतः पाँचवी कक्षा में नाम लिखने के लिए हेडमास्टर साहब को ही आविष्कृत करनी पड़ी-6 जुलाई, 1947।
इसके पूर्व परिवार की अदनी इकाई के रूप में नाक चुआता, मक्खियों की भिनभिनाहट धूल-गंन्दगी में डोलता एक बच्चा था जिसके लिए पैंट, भगवे, पढ़ाई-लिखाई की कोई समस्या नहीं थी तब। मैं उन दिनों नंगधड़ंग सियारों, नीलगायों, लोमड़ियों, गिलहरियों को जिज्ञासु नज़रों से जाँचता-परखता, भैंस की पीठ पर चरागाहों की सैर किया करता। केले की छाल का पनही, पलास के पत्तों को टोप, कई की क्रूई की कंठी, सोते का पानी।
बहरहाल गाँव से काका ले आए कुल्टी इंडियन आयरन एंड स्टील कं. के पिछड़े औद्योगिक कस्बे में। एक डर काकी, का, दूसरा भैया का जिन्हें भैंस की पीठ पर काफी उम्र गुजारने के बाद ही पढ़ने की स्वीकृति मिल पाई थी। वे आगे-आगे चल रहे थे मैं पीछे-पीछे-कई कक्षाओं के अन्तराल पर उसका अनुसरण कर रहा था। इसी भय के कारण पहली बार इम्तिहान-नुमा चीज़ की हल की गई पुस्तिका जमा करने की बजाय भैया की जबावदेही से बचने के लिए मास्टरो से छिपकर सरपट भागता हुआ उनके (भैया के) हवाले कर बैठा तो उन्होंने सर पीट लिया ! भूलने से बचने के लिए सारी कापी किताबें एक साथ नत्थी कर दी गई थीं। जिन्हें एक भीषण वर्षा में, नाले के हवाले कर आया। कई चुल्लू पानी पीकर उठा तो सब साफ। पढ़ाई अब गुरूजी की पाठशालाओं में होने लगी, जहाँ पढ़ने और भेड़ों की तरह सर लड़ाने में एक जैसी ख्याति हासिल की। सज़ा के रूप में मूर्ख मॉनीटर सूरज की ओर ताकते रहने को कहता । भैया हाँकने रहने से जब किसी तरह पाँचवीं जमात की शाला में दाखिला मिला तो एक दूसरी दुनियाँ खुली-पढ़ाई और धर्म का समन्वय। हनुमान-चालीसा और देवी-देवताओं की स्तुतियाँ तो बड़े भैया रामसेवक का पाठ सुन-सुनकर ही याद थे। बाकी कमी पूरा की भागवत, राधेश्याम-रामायण पाठ के लिए। सुन-सुनकर ही याद थे। बाकी कमी गीता, प्रेम सागर, सुख सागर की आरोपित, आदर्श भक्ति द्वारा कठिनाइयों के समाधान की तलाश ! जासूसी उपन्यासों द्वारा आरोपित नायकत्व !
यूँ तो साहित्य जगाने का श्रेय वरिष्ठ मित्र नरेन्द्रनाथ ओझा को जाता है, पर शुरू-शुरू में साहित्य के क्षेत्र में चारा देकर ही बुलाया गया था। ड्रिल का पीरियड था। उस दिन ड्रिल कराने की फुर्सत नहीं थी मास्टर साहब अनिल कुमार महथा जी को, सो सिविल के पुरस्कार की ‘ड्रिल पर कविता प्रतियोगिता’। तब से जाने कितने पुरस्कार। तुकबन्दी आगे चलकर अंताक्षरी में भी काम आती। सातवीं कक्षा में पहला भाषण गांधीजी पर रटा-रटाया; फिर तुलसी जयन्तियाँ वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ। मौसमी लेखन के बीच में ऊलजलूल लेखन भी। जैसे सहपाठी साथी ‘सूरज’ के साथ प्रधानमन्त्री को पत्र लिखना-प्रधानमंत्री जी देश की हालत बड़ी खराब होती जा रही है। सूरज का तो जल्द ही धर्म, सत्ता और व्यवस्था से मोह-भंग होता गया। मैं काफी भटकर उसके द्वारा अपनाई गई मार्क्सवादी राह पर आया था। धर्म के सहभागियों द्वारा धीरे-धीरे कुछ कुटेवों के दलदल में भी फँसा। शुकर था जल्द ही निकल आया। फल यह हुआ कि स्कूल का अभी फ्रर्स्ट ब्वाय’ मैट्रिक में सेंकेंड डिवीज़न में उत्तीर्ण हुआ। गाँव अभी भी जुड़ जाता बीच-बीच में जहाँ दो-दो कोस पर नाच देखने चल देता रात को और दिन को खेती के काम।
अब काँलेज ! इच्छा के विरुद्ध विज्ञान का छात्र बना दिया गया। भाषा के प्रति मोह बढ़ रहा था। प्रकृति के रूपों में उलझा-उलझा मन ! पन्त प्रिय कवि। प्रेमचन्द्र, सुदर्शन, शिवपूजन सहाय, पदुमलाल पुन्नालाल बक्षी की रचनाओं से अनुप्रेरित होकर पहली हृदय-परिवर्तन की कहानी हस्तलिखित पत्रिका ‘पल्लव’ में। मौसमी लेखन में कविता, कहानी निबन्ध के पुरस्कार। भैया बनाना चाहते थे डाक्टर, इन्जीनियर। पैसे की औकात रत्ती-भर की नहीं थी और फिर मुझे, मेढक, मछलियों को देखकर घिन आती, काटना तो दूर, छूना भी गवारा नहीं। इन्जीनियरिगं में टेस्ट की जगह अपनी दूसरी परीक्षाएँ ध्यान खींच ले जातीं मार्क्स के आधार पर दो-एक जगह सम्भावना जगी तो आयु आड़े आ गई। खैर सत्रह साल की वय में बी.एस–सी. डिस्टिंक्शन से पासकर भैया ने मुझे दिल्ली भेजा ए.एम.आई.ई. पढ़ने को। पायजामे से निकालकर पैंट की दुनियाँ अधखाए परिवार के पेट पर एक इंजीनियर खड़ा करने की कोशिश।
इस बीच वैचारिक स्तर पर काफी कुछ बदलता रहा था। रामलीला, रासलीला कब छूटी और बंगला के जात्रा, नाटक, स्वस्थ फिल्में कब आ लगे, पता नहीं। सुमन वृन्त और जालों पर झिलमिलाते तुहिन बिन्दु कब श्रम सीकरों द्वारा विस्थापित हो गए। ट्रेन में जगकर उस क्षण की प्रतीक्षा करना कि कब काली रात भोर की लाली की ते़ज़ाबी तासीर में घुलती है वह रहस्य कब चुपके-चुपके खुल गया पता नहीं !
बाहर की दुनिया से जोड़ने का श्रेय मित्र बलराम को है। शुरू-शुरू में काफी संघर्ष आज की मेरी चर्चित कहानी भी तब वापस कर दी जाती। कमलेश्वर जी पत्र द्वारा प्रेरणा देते रहते। सुभाष पन्त का खत आता। इन्हीं दिनों पढ़ गया चेखव, दोस्तोएवस्की, गोर्की, तोल्स्तोय, ओ हेनरी लू–सुन, रवीन्द्र, शरत, सार्त्र, कामू काफ्का आदि को।
ज़िन्दगी के सबसे बड़े संबल हैं मित्र-दूर-दूर तक फैले हुए। जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा कद्र करता हूँ वे भगत सिंह, जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वह आदमी का कमीनापन। जातिवाद, सामन्वाद, पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, इसी कमीनेपन के फूल हैं और मेरे लेखन के ये ही निशाने रहेंगे। स्वीकारने में शर्म नहीं कि मेरा लेखन उद्देश्यपरक है। इस उद्देश्य के लिए कोई भी मंच, संप्रेषण की कोई भी तकनीक के माध्यम अपनाने को तैयार हूँ। जहाँ तक साहित्य की बात है, जनजीवन के बीच उतरने में अगर उसकी धोती मैली होती है तो हो, मगर उसे उतारकर ही रहता हूँ।
अपने पति कोई मुगालता नहीं हैं। लेखक होने के नाते किसी विषय सुविधा की मांग भी नहीं करता जिस देश के तीन-चौथाई बूढ़े से लेकर बच्चे तक दिन-रात जांगर पेरकर भी भूख, अभाव, दमन और जलालत की ज़िन्दगी जीते रहे हैं वहाँ एक रचानाकार की गर्दिश को उछाला जाना वाहियात बात है। इस लिहाज से रोटी खाना और कपड़े पहनना तक अपराध लगने लगता है कभी-कभी लेकिन बेहया....बनकर रहा हूँ। शायद बोल्ड ही नहीं हूँ, अगर होता तो लिखने कि बजाए कुछ और कर रहा होता। साथी सूरज इस बीच शहीद हो चुके हैं।
एक कथाकार के रूप में महसूस करता हूँ कि कहानी जहाँ खत्म होती है, वहीं उसकी वास्वविक शुरूआत होती है। जब तक विचार कार्य में नहीं ढलते, कहानी का उदेश्य पूरा नहीं होता। इतना सारा कुछ तो लिखा गया, मगर वह बरसात के नम बम-सा क्या कर पाया ? शायद इसी कचोट को तोल्स्तोय ने अपने अन्तिम दिनों में गोर्खी से व्यक्त किया था, ‘‘इतना लिखा गया मगर कुछ नहीं हुआ, दुनिया पहले की अपेक्षा की हुई हैं, ‘फिर भी.....’’
जीवन के निबन्ध व्याकरण ने कितनी ही संज्ञाएँ दीं- संजीवन, संजीवन, सजेवन, साजन, सजावन और संजीव। इन तत्सम, तद्भव, देशज. विदेशज (?) नामों के साथ राम और प्रसाद के उपमार्ग-प्रत्यय और ‘मास्टर’ का सर्वनाम-विश्लेषण। जन्म की तिथि मेरे जैसे परिवार के लिए कोई महत्त्व की बात नहीं थी, अतः पाँचवी कक्षा में नाम लिखने के लिए हेडमास्टर साहब को ही आविष्कृत करनी पड़ी-6 जुलाई, 1947।
इसके पूर्व परिवार की अदनी इकाई के रूप में नाक चुआता, मक्खियों की भिनभिनाहट धूल-गंन्दगी में डोलता एक बच्चा था जिसके लिए पैंट, भगवे, पढ़ाई-लिखाई की कोई समस्या नहीं थी तब। मैं उन दिनों नंगधड़ंग सियारों, नीलगायों, लोमड़ियों, गिलहरियों को जिज्ञासु नज़रों से जाँचता-परखता, भैंस की पीठ पर चरागाहों की सैर किया करता। केले की छाल का पनही, पलास के पत्तों को टोप, कई की क्रूई की कंठी, सोते का पानी।
बहरहाल गाँव से काका ले आए कुल्टी इंडियन आयरन एंड स्टील कं. के पिछड़े औद्योगिक कस्बे में। एक डर काकी, का, दूसरा भैया का जिन्हें भैंस की पीठ पर काफी उम्र गुजारने के बाद ही पढ़ने की स्वीकृति मिल पाई थी। वे आगे-आगे चल रहे थे मैं पीछे-पीछे-कई कक्षाओं के अन्तराल पर उसका अनुसरण कर रहा था। इसी भय के कारण पहली बार इम्तिहान-नुमा चीज़ की हल की गई पुस्तिका जमा करने की बजाय भैया की जबावदेही से बचने के लिए मास्टरो से छिपकर सरपट भागता हुआ उनके (भैया के) हवाले कर बैठा तो उन्होंने सर पीट लिया ! भूलने से बचने के लिए सारी कापी किताबें एक साथ नत्थी कर दी गई थीं। जिन्हें एक भीषण वर्षा में, नाले के हवाले कर आया। कई चुल्लू पानी पीकर उठा तो सब साफ। पढ़ाई अब गुरूजी की पाठशालाओं में होने लगी, जहाँ पढ़ने और भेड़ों की तरह सर लड़ाने में एक जैसी ख्याति हासिल की। सज़ा के रूप में मूर्ख मॉनीटर सूरज की ओर ताकते रहने को कहता । भैया हाँकने रहने से जब किसी तरह पाँचवीं जमात की शाला में दाखिला मिला तो एक दूसरी दुनियाँ खुली-पढ़ाई और धर्म का समन्वय। हनुमान-चालीसा और देवी-देवताओं की स्तुतियाँ तो बड़े भैया रामसेवक का पाठ सुन-सुनकर ही याद थे। बाकी कमी पूरा की भागवत, राधेश्याम-रामायण पाठ के लिए। सुन-सुनकर ही याद थे। बाकी कमी गीता, प्रेम सागर, सुख सागर की आरोपित, आदर्श भक्ति द्वारा कठिनाइयों के समाधान की तलाश ! जासूसी उपन्यासों द्वारा आरोपित नायकत्व !
यूँ तो साहित्य जगाने का श्रेय वरिष्ठ मित्र नरेन्द्रनाथ ओझा को जाता है, पर शुरू-शुरू में साहित्य के क्षेत्र में चारा देकर ही बुलाया गया था। ड्रिल का पीरियड था। उस दिन ड्रिल कराने की फुर्सत नहीं थी मास्टर साहब अनिल कुमार महथा जी को, सो सिविल के पुरस्कार की ‘ड्रिल पर कविता प्रतियोगिता’। तब से जाने कितने पुरस्कार। तुकबन्दी आगे चलकर अंताक्षरी में भी काम आती। सातवीं कक्षा में पहला भाषण गांधीजी पर रटा-रटाया; फिर तुलसी जयन्तियाँ वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ। मौसमी लेखन के बीच में ऊलजलूल लेखन भी। जैसे सहपाठी साथी ‘सूरज’ के साथ प्रधानमन्त्री को पत्र लिखना-प्रधानमंत्री जी देश की हालत बड़ी खराब होती जा रही है। सूरज का तो जल्द ही धर्म, सत्ता और व्यवस्था से मोह-भंग होता गया। मैं काफी भटकर उसके द्वारा अपनाई गई मार्क्सवादी राह पर आया था। धर्म के सहभागियों द्वारा धीरे-धीरे कुछ कुटेवों के दलदल में भी फँसा। शुकर था जल्द ही निकल आया। फल यह हुआ कि स्कूल का अभी फ्रर्स्ट ब्वाय’ मैट्रिक में सेंकेंड डिवीज़न में उत्तीर्ण हुआ। गाँव अभी भी जुड़ जाता बीच-बीच में जहाँ दो-दो कोस पर नाच देखने चल देता रात को और दिन को खेती के काम।
अब काँलेज ! इच्छा के विरुद्ध विज्ञान का छात्र बना दिया गया। भाषा के प्रति मोह बढ़ रहा था। प्रकृति के रूपों में उलझा-उलझा मन ! पन्त प्रिय कवि। प्रेमचन्द्र, सुदर्शन, शिवपूजन सहाय, पदुमलाल पुन्नालाल बक्षी की रचनाओं से अनुप्रेरित होकर पहली हृदय-परिवर्तन की कहानी हस्तलिखित पत्रिका ‘पल्लव’ में। मौसमी लेखन में कविता, कहानी निबन्ध के पुरस्कार। भैया बनाना चाहते थे डाक्टर, इन्जीनियर। पैसे की औकात रत्ती-भर की नहीं थी और फिर मुझे, मेढक, मछलियों को देखकर घिन आती, काटना तो दूर, छूना भी गवारा नहीं। इन्जीनियरिगं में टेस्ट की जगह अपनी दूसरी परीक्षाएँ ध्यान खींच ले जातीं मार्क्स के आधार पर दो-एक जगह सम्भावना जगी तो आयु आड़े आ गई। खैर सत्रह साल की वय में बी.एस–सी. डिस्टिंक्शन से पासकर भैया ने मुझे दिल्ली भेजा ए.एम.आई.ई. पढ़ने को। पायजामे से निकालकर पैंट की दुनियाँ अधखाए परिवार के पेट पर एक इंजीनियर खड़ा करने की कोशिश।
इस बीच वैचारिक स्तर पर काफी कुछ बदलता रहा था। रामलीला, रासलीला कब छूटी और बंगला के जात्रा, नाटक, स्वस्थ फिल्में कब आ लगे, पता नहीं। सुमन वृन्त और जालों पर झिलमिलाते तुहिन बिन्दु कब श्रम सीकरों द्वारा विस्थापित हो गए। ट्रेन में जगकर उस क्षण की प्रतीक्षा करना कि कब काली रात भोर की लाली की ते़ज़ाबी तासीर में घुलती है वह रहस्य कब चुपके-चुपके खुल गया पता नहीं !
बाहर की दुनिया से जोड़ने का श्रेय मित्र बलराम को है। शुरू-शुरू में काफी संघर्ष आज की मेरी चर्चित कहानी भी तब वापस कर दी जाती। कमलेश्वर जी पत्र द्वारा प्रेरणा देते रहते। सुभाष पन्त का खत आता। इन्हीं दिनों पढ़ गया चेखव, दोस्तोएवस्की, गोर्की, तोल्स्तोय, ओ हेनरी लू–सुन, रवीन्द्र, शरत, सार्त्र, कामू काफ्का आदि को।
ज़िन्दगी के सबसे बड़े संबल हैं मित्र-दूर-दूर तक फैले हुए। जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा कद्र करता हूँ वे भगत सिंह, जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वह आदमी का कमीनापन। जातिवाद, सामन्वाद, पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, इसी कमीनेपन के फूल हैं और मेरे लेखन के ये ही निशाने रहेंगे। स्वीकारने में शर्म नहीं कि मेरा लेखन उद्देश्यपरक है। इस उद्देश्य के लिए कोई भी मंच, संप्रेषण की कोई भी तकनीक के माध्यम अपनाने को तैयार हूँ। जहाँ तक साहित्य की बात है, जनजीवन के बीच उतरने में अगर उसकी धोती मैली होती है तो हो, मगर उसे उतारकर ही रहता हूँ।
अपने पति कोई मुगालता नहीं हैं। लेखक होने के नाते किसी विषय सुविधा की मांग भी नहीं करता जिस देश के तीन-चौथाई बूढ़े से लेकर बच्चे तक दिन-रात जांगर पेरकर भी भूख, अभाव, दमन और जलालत की ज़िन्दगी जीते रहे हैं वहाँ एक रचानाकार की गर्दिश को उछाला जाना वाहियात बात है। इस लिहाज से रोटी खाना और कपड़े पहनना तक अपराध लगने लगता है कभी-कभी लेकिन बेहया....बनकर रहा हूँ। शायद बोल्ड ही नहीं हूँ, अगर होता तो लिखने कि बजाए कुछ और कर रहा होता। साथी सूरज इस बीच शहीद हो चुके हैं।
एक कथाकार के रूप में महसूस करता हूँ कि कहानी जहाँ खत्म होती है, वहीं उसकी वास्वविक शुरूआत होती है। जब तक विचार कार्य में नहीं ढलते, कहानी का उदेश्य पूरा नहीं होता। इतना सारा कुछ तो लिखा गया, मगर वह बरसात के नम बम-सा क्या कर पाया ? शायद इसी कचोट को तोल्स्तोय ने अपने अन्तिम दिनों में गोर्खी से व्यक्त किया था, ‘‘इतना लिखा गया मगर कुछ नहीं हुआ, दुनिया पहले की अपेक्षा की हुई हैं, ‘फिर भी.....’’
संजीव
सर्कस
सौ से डेढ़ सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हरहराती उड़ी चली जा रही थीं हवाएँ बूँदों का आँचल छहराते हुए, ‘हा-हा, हू-हू, सों-सों !’ टेलीग्राफ और बिजली के तारों को छेड़कर महाकाल बजा रहा था सायरन ! अपने प्रबल उन्माद में झंझा रह-रहकर चक्रवात में रूपान्तरित हो उठती, तब लगता की तम्बू-तम्बू उखड़कर हवा में गुब्बारे की तरह उड़ जाएगा। विभाजित व्यक्तित्व के मानिन्द एक ओर बूँदों की सेना दूसरी ओर की सेना से टकराकर धुँआ बनकर बिखर जाती। और वे धीरोचित पेड़ ! आज उनकी ख़ैर नहीं किसी गुंडावाहिनी की तरह उनके बाल पकड़कर नचा रही थी झंझा ! चाबुक सटकाते हुए !
‘सों-सों’ की एक जोरदार आवाज़ हुई और इसके साथ ही ‘कामिनी-कलाभवन’ का साइनबोर्ड किसी परिन्दे के कटे पर की तरह दूर जा उड़ा। इसके साथ ही कई और कला टिन की शीटों की किलेबन्दी के परखचे उड़े, बिजली के तारों पर अर्जुन वृक्ष की बड़ी डाल अरराकर गिरी और घुप्प अँधेरे में प्लेन क्रैश का-सा धमाका और गरमराहट बड़ी देर तक पानी और हवा के रेले में पछाड़ खती रही। रोशनी के नाम पर बस बची हुई थी बिजली की लापरवाही कौंध, जिसकी तड़प लगता था आकाश को ही नहीं पृथ्वी को भी चाक कर जाएगी।
‘‘यह क्या ! तम्बू फट गया। पानी हरहाराकर गिरने लगा अन्दर। हटाओ, हटाओ; उधर के समान हटाओ। काट दो स्विच कहीं करंट आ गया तो शॉक लग जाएगा। अरे बाँस ले आओ जल्दी। वहाँ मर गए ? टार्च है कहाँ, टार्च, बचो, वह रोला गिरा ! हाय!’
‘सों-सों’ की एक जोरदार आवाज़ हुई और इसके साथ ही ‘कामिनी-कलाभवन’ का साइनबोर्ड किसी परिन्दे के कटे पर की तरह दूर जा उड़ा। इसके साथ ही कई और कला टिन की शीटों की किलेबन्दी के परखचे उड़े, बिजली के तारों पर अर्जुन वृक्ष की बड़ी डाल अरराकर गिरी और घुप्प अँधेरे में प्लेन क्रैश का-सा धमाका और गरमराहट बड़ी देर तक पानी और हवा के रेले में पछाड़ खती रही। रोशनी के नाम पर बस बची हुई थी बिजली की लापरवाही कौंध, जिसकी तड़प लगता था आकाश को ही नहीं पृथ्वी को भी चाक कर जाएगी।
‘‘यह क्या ! तम्बू फट गया। पानी हरहाराकर गिरने लगा अन्दर। हटाओ, हटाओ; उधर के समान हटाओ। काट दो स्विच कहीं करंट आ गया तो शॉक लग जाएगा। अरे बाँस ले आओ जल्दी। वहाँ मर गए ? टार्च है कहाँ, टार्च, बचो, वह रोला गिरा ! हाय!’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book