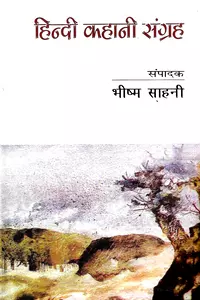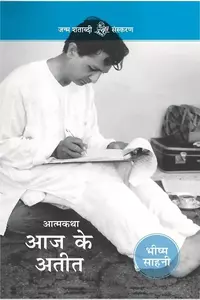|
उपन्यास >> बसंती बसंतीभीष्म साहनी
|
259 पाठक हैं |
|||||||
भीष्म साहनी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक
Basanti a hindi book by Bhisham Sahni - बसंती - भीष्म साहनी
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
झरोखे, कड़ियाँ और तमस जैसे तीन विभिन्न आयामी उपन्यासों के बाद बसंती का आना भीष्म साहनी के निर्बंध कथाकार की एक और सृजनात्मक उपलब्धि है। भीष्मजी ने इस उपन्यास में एक ऐसी लड़की का चित्रण किया है जो मेहनत-मजदूरी करने के लिए महासागर में आए ग्रामीण परिवार की कठिनाईयों के साथ-साथ बड़ी होती है; और निरंतर ‘बड़ी’ होती जाती है।
दिल्ली जैसे महानगर में नए-नए और कॉलोनियाँ उठानेवालों की आए दिन टूटती झुग्गी-बस्तियों में टूटते गरीब लोगों, रिश्ते-नातों, सपनों और घरौंदों के बीच मात्र बसंती ही है जो साबुत नजर आती है। वह अपने परिवार, परिवेश और परंपरागत नैतिकता से विद्रोह करती है और चाहे यह विद्रोह उसे दैहिक और मानसिक शोषण तक ही ले जाता है, पर उसकी निजता का कोई हादसा तोड़ नहीं पाता। प्रेमिका और ‘पत्नी’ के रूप में कठिन-से-कठिन हालात को तो क्या बीबी जी कहकर उड़ाने और खिलखिलाने में ही जैसे बसंती की सार्थकता है। दूसरे शब्दों में वह एक जीती-जागती जिजीविषा है।
अपने आस-पास के सामाजिक यथार्थ को उसके समूचेपन में उद्धघाटित करनेवाले अप्रतिम कथाकार भीष्म साहनी का यह उपन्यास महानगरीय जीवन की खोखली चमक-दमक और ठोस अँधेरी खाइयों के बीच भटकती बसंती जैसी एक पूरी पीढ़ी का शायद पहली बार प्रभावी चरित्रांकन प्रस्तुत करता है
दिल्ली जैसे महानगर में नए-नए और कॉलोनियाँ उठानेवालों की आए दिन टूटती झुग्गी-बस्तियों में टूटते गरीब लोगों, रिश्ते-नातों, सपनों और घरौंदों के बीच मात्र बसंती ही है जो साबुत नजर आती है। वह अपने परिवार, परिवेश और परंपरागत नैतिकता से विद्रोह करती है और चाहे यह विद्रोह उसे दैहिक और मानसिक शोषण तक ही ले जाता है, पर उसकी निजता का कोई हादसा तोड़ नहीं पाता। प्रेमिका और ‘पत्नी’ के रूप में कठिन-से-कठिन हालात को तो क्या बीबी जी कहकर उड़ाने और खिलखिलाने में ही जैसे बसंती की सार्थकता है। दूसरे शब्दों में वह एक जीती-जागती जिजीविषा है।
अपने आस-पास के सामाजिक यथार्थ को उसके समूचेपन में उद्धघाटित करनेवाले अप्रतिम कथाकार भीष्म साहनी का यह उपन्यास महानगरीय जीवन की खोखली चमक-दमक और ठोस अँधेरी खाइयों के बीच भटकती बसंती जैसी एक पूरी पीढ़ी का शायद पहली बार प्रभावी चरित्रांकन प्रस्तुत करता है
एक
सुबह सवेरे जब चौधरी अपनी कोठरी से निकला तो हवा में कोहरा छाया था—नील-मायल धुँधला-सा कोहरा जो किसी दिन सुबह उठो तो अकारण ही चारों ओर नजर आने लगता है। और साथ ही चुभोती ठंडी हवा। उसने आँख उठाकर ऊपर की ओर देखा-मटमैल बादल, जैसे रात-ही-रात में नीचे उतर आए थे। इसी कारण सवेरा हो जाने पर भी दिन का गुमान नहीं होता था। ‘बरसेगा, आज जरूर बरसेगा’, चौधरी बुदबुदाया। पर बस्ती जाग गई थी और दिन का व्यापार छिट-पुट
शुरू हो गया था। बगलवाली कोठरी में से बिसेसर की पत्नी जमुना, सिर पर घड़ा रखे नल पर से पानी लेने के लिए निकली और ढलान चढ़ने लगी। ऊपर बड़े नल के ही पास, ढलान के सिरे पर गोबिंदी की चाय पानी की दूकान खुल गई थी, घनी धुँघ में से भी उसकी बत्ती की लौ नजर आ रही थी। चौधरी ने घूमकर, ढलान के नीचे नजर दौड़ाई। ऊबड़-खाबड़ गली के दोनों ओर खड़ी छोटी-छोटी कोठरियों में भी हरकत शुरू हो गई थी। किसी-किसी कोठरी के बाहर चूल्हा जलने लगा था। कहीं-कहीं बस्ती की कोई लड़की, चादर में मुँह सिर लपेटे, ढलान उतरती हुई, बस्ती के बाहर लोगों के घरों में चौका बर्तन करने जा रही थी। बाहर की बड़ी सड़क अभी से चलने लगी थी, दूर से लारियों-मोटरों के भोंपुओं की आवाजें, धुंध और कोहरे में लिपटी-सी सुनाई पड़ने लगी थीं।
हर बार, बारिश का समा होने पर चौधरी बड़बड़ाता था। आज तो धुंध भी थी और बादल भी घिरे थे जो न जाने कब बरसने लगें। आज तो अपने अड्डे पर जाने में कोई तुक नहीं, कौन इस मौसम में बाल कटवाने या हजामत बनवाने आएगा। आज का दिन भी बर्बाद गया समझो। उसका मन हुआ, बैठकर बीड़ी सुलगा ले। उसने अपने नीले कुर्ते की जेब से बीड़ी निकाली भी, पर फिर अपनी ही कोठरी के बाहर बैठने के बजाए बाहर निकल आया और गोबिंदी की चाय की दूकान की ओर कदम बढ़ा दिए। कल हीरा और धन्ना और बस्ती के कुछ और लोग हकीम से मिलने गए थे, दिन-भर बाहर बने रहे, कुछ पता तो चले, स्याह-सफेद क्या कर आए हैं। सरकार ने क्या कहा है, क्या फैसला दिया है। सुबह सवेरे, हर रोज, अपने-अपने काम पर जाने से पहले, कुछ देर के लिए, गोबिंदी की दूकान में छोटा-मोटा जमाव जरूर होता था। कुछ लोग तो जरूर वहाँ बैठे होंगे।
जब चौधरी गोबिंदी के चाय-घर के पास पहुँचा तो सचमुच वहाँ जमाव था, और दूर से ही हीरा की आवाज सुनाई पड़ रही थी, ऊँची आवाज में बोल रहा था, ‘‘हमने हाथ बाँधकर कहा, ‘‘मालिक हम राज-मिस्त्री हम ही घर बनावैं और हमारे ही रहने को ठौर नहीं, लोगों को घर जुटावैं और अपना सिर छिपाने के लिए जगह ही नहीं। इस मेंह-बरसात में तो हमें बेघर नहीं करो।’’
‘‘फिर हाकिम क्या बोला ?’’ किसी की आवाज आई। ‘‘हाकिम भला लोग था। बड़े धीरज से बात सुनता रहा। बड़े अफसर तो भले लोग ही होते हैं, हरामी तो नीचेवाले छोटे अफसर होते हैं।’’...हीरा कह रहा था।
तभी चौधरी ने चाय घर में कदम रखा।
‘‘क्या कर आए हो, हीरा ? हाकिम लोग मान गए ?’’ कहते हुए चौधरी चबूतरे पर बैठ गया। चाय घर में बस्ती के सात-आठ आदमी बैठ थे। हीरा अभी भी सिर पर राजस्थानी पग्गड़ बाँधे और कलवाले ही उजले कपड़े और काली बास्कट पहने था जिन्हें पहनकर वहा हाकिमों से मिलने गया था।
चौधरी के अंदर आ जाने पर भी चाय घर में बैठे लोगों ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। बरसों से इस बस्ती के छोर पर रहने के बावजूद उसे अभी भी बाहर का, छोटी जात का आदमी ही माना जाता था। चौधरी अहीर था जबकि ये लोग राजस्थानी थे। फिर वह नौवा, और ये राज-मजदूर राज-मिस्त्री। वह अपनी जात-बिरादरी से कटा हुआ—बस्ती में तीन-चार ही घर अहीरों के थे, और वे भी एक-दूसरे से फटे हुए—जबकि इन लोगों की पूरी बिरादरी थी,
अपनी पंचायत थी, ये लोग आपस में गठे हुए थे। चौधरी के सवाल की तरफ विशेष ध्यान न देते हुए, हीरा मिस्त्री कहे जा रहा था, ‘‘बात तो तब बिगड़ी जब बड़े साहिब ने हमें छोटे अफसर के सुपुर्द कर दिया, कि इनसे बात करो, यह तुम्हें सब बात समझा देंगे। बस, तभी बात बिगड़ी। सच पूछो, तो जब यह छोटा अफसर अंदर घुसा तो मेरे अंदर से आवाज आई हीरा, मामला बिगड़ गया है। मालिक ने जैसे गाय की रस्सी अपने हाथों से कसाई के हाथ में दे दी हो। अंदर से ही जैसे फुरनी फुरती है, मुझे पता चला गया कि मामला बिगड़ गया है।’’
‘‘क्यों ?’’
‘‘क्यों क्या ? छोटे अफसर ने हमें बोलने ही नहीं दिया-हमें अपने दफ्तर में ले गया और फैसला सुना दिया-तुम्हें निकलना होगा, बस्ती खड़ी नहीं रह सकती। पूछो रामपरकाश से। इसने कुछ कहने को मुँह खोला कि वह अफसर कड़ककर बोला, सरकार ने जो फैसला करना था, कर दिया। अब बहस करने की कोई जरूरत नहीं।’ लो सुनो, यह भी कोई बोलने का ढंग है। अरे बोलो तो मीठा, काम तो होगा,
नहीं होगा, यह तो भगवान के हाथ है, पर बोलो तो मीठा। हमसे कड़वा बोलकर तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारे भाग अच्छे थे, तुम अफसर बन गए। हमारे भाग खोटे थे, हम मिस्त्री-मजूर बने, पर भाई बोलो तो मीठा। हमारा पानी तो नहीं उतारो हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं, हमारी पगड़ी तो न हीं उछालो। हमारे बाप-दादा भी जमीन-जायदादवाले थे, अभी भी राजस्थान में हमारी अपनी खेती है। अब वहाँ सूखा पड़े तो हम क्या करें ? बाल-बच्चों का पेट पालने के लिए दिल्ली चले आए। पर हमारे साथ बोलो तो मीठा !’’
किसी गीत की स्थायी पंक्ति की भाँति हीरा बार-बार यही वाक्य दोहराए जा रहा था-बोलो तो मीठा, भाई हमारे साथ बोलो तो मीठा !
चौधरी समझ गया कि मामला बिगड़ गया है। पिछले दिन, बस्ती के तीन और लोगों को साथ लेकर हीरा ‘सरकार’ से मिलने गया था। पूरा राजस्थानी बाना पहनकर तीनों जने गए थे। सिर पर पग्गड़ आँखों में काजल घेरेदार ‘अँगरखा’ और तेल-चिपुड़ी लाठी हरेक के हाथ में थी। चौधरी ने ही तीनों की हजामत भी बनाई थी, और चलते समय हँसी-हँसी में कहा भी था, ‘‘अब काजल सुरमा लगाकर चले हो तो काम निबटाकर लौटना।
पहले की तरह खाली हाथ नहीं लौट आना। पर उधर अफसर ने बिना बात सुने चलता कर दिया था और धमकी दी थी कि चपरासी को बुलाकर बाहर निकाल देगा।
‘‘हाकिम अच्छा मिल जाए, यह भी किस्मत की बात होती है। पिछली बार जब बस्ती तोड़ने की बात चली थी, तो हम जिस साहिब से मिले थे, वह तो घंटे तक हमारी बात सुनता रहा और मामला आगे नहीं बढ़ने दिया था।’’
‘‘तुम कल भी उसी अफसर से जा मिलते, उसके सामने हाथ जोड़ते।’’
‘‘यही तो कहा, किस्मत खोटी हो तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। उसी के दफ्तर में तो गए थे। पर वह अब वहाँ पर नहीं बैठता। किसी दूसरे दफ्तर में काम करता है। उससे मेल-मुलाकात हो जाती तो जरूर कोई रास्ता निकल आता।’’
‘‘अब क्या कर आए हो ?’’
‘‘हम क्या करेंगे ? हाथ बाँधकर गए थे, हाथ बाँधकर ही लौट आए।’’
‘‘वह नहीं तो किसी दूसरे अफसर से मिलो। किसी मंतरीजी सेमिलो।’’
इस पर मूलराज बोला, ‘‘हमने पहले ही कहा था, पक्के घर यहाँ नहीं बनाओ, न तुम्हारी जमीन, न तुम्हारे नाम का पट्टा।’’
"दस-बीस रोज की बात होती तो कच्ची झोंपड़ियों में पड़े रहते। अब तो यहाँ रहते भी बरसों बीत गए। घर पक्का बना लिया तो क्या गुनाह किया।"
मूलराज लोहे की कुर्सी के ऊपर दोनों पाँव चढ़ाए बैठा था, और बीड़ी के कश ले रहा था। कल रोज घिरे बादलों के बावजूद वह एक घर में पुताई का काम करता रहा था, और पुताई के छींटे अभी भी उसके हाथों और पाँवों पर पड़े थे। एकाध छींटा उसके मुँह पर भी मौजूद था।
"तो क्या कहते हो, आज काम पर नहीं जाएँ ?"
"नहीं, काम पर क्यों नहीं जाएँ। यह काम इतनी जल्दी थोड़े ही निबटते हैं। हमें यहाँ से निकालेंगे भी तो महीना-दो महीना तो लग ही जाएगा। अभी कागज ऊपर जाएँगे।"
"यह पहली बार तो बस्ती गिराने की बात नहीं हुई ना, कई बार पहले भी हो चुकी है। क्या मालूम अबकी बार भी बस्ती बच जाए। हाकिम के दिल की कौन जाने।"
"उन्होंने महीने-भर का नोटिस दिया था, वह तो खत्म हो गया।" चौधरी ने अपनी छोटी-छोटी शंकित आँखों से देखते हुए कहा।
"नोटिस की बात नहीं करो, वे तो आए दिन मिलते रहते हैं।"
खौलती चाय की केतली के पास बैठी गोबिंदी बोली, "तुम मर्द लोग डरते काँपते ही रहोगे। अबकी बार अफसर से मिलने जाओ तो मुझे साथ ले चलना। अफसर को ऐसी फटकार सुनाऊँगी कि नानी याद करा दूँगी।"
"तू क्या कहेगी, रानी ?"
"मैं कहूँगी, जिस जमीन पर हमारी कोठरियाँ खड़ी हैं, वे हमारे नाम कर दो। और हमसे जमीन के पैसे ले लो। कोठरियाँ तो हमने अपने पैसों से बनाई हैं, इन्हें कोई क्यों तोड़े ? हमारा नुकसान भी करें और हमें बेघर भी करें। तुम्हारे मुँह से बात ही नहीं निकलती। अँगरखे पहने कचहरी में मटक-मटककर आ गए।"
"कहती तो ठीक हो", मूलराज ने कहा, "हीरा, हमें यही कहना चाहिए था।"
"अरे, कोई बात सुने तब ना। पहले यह नहीं कहा था ? यही तो बरसों से कहते आ रहे हैं। कोई सुने तो। हम एक नहीं, दस तरकीबें बतावैं। हम अनाड़ी तो नहीं हैं, हमारे हाथ से बीसियों घर बने हैं।"
"आज फिर चले चलो, गोबिंदी को भी ले चलो। क्यों हीरा ? तुमने तो अभी अपने वस्तर भी नहीं उतारे।" चौधरी ने मसखरी करते हुए कहा।
हीरा ने हल्के-से सिर हिलाया, "कोई अच्छा अफसर मिल जाए तो बात बन जाए।"
चौधरी चुपचाप चबूतरे पर से उठकर बाहर आ गया।
बस्ती क्या थी, दिल्ली की ही एक सड़क के किनारे छोटा सा राजस्थान बना हुआ था। आजादी के बाद, दिल्ली शहर फैलने लगा था। नई-नई बस्तियों की उसारी होने लगी थी और उन बस्तियों को बनाने के लिए जगह-जगह से राज-मजदूर खिंचे आने लगे थे। दिल्ली से दूर, जहाँ कहीं सूखा पड़ता या बाढ़ आती, वहीं से लोग उठ-उठकर दिल्ली की ओर भागने लगते। कहीं परिवार के परिवार चले आए, कहीं अकेले मर्द कहीं छोटी उम्र के लौंडे लड़के भी। कहीं राजस्थान से तो कहीं हरयाणा और पंजाब के गाँवों से, और कहीं तो दूर दक्षिण से भी; पर राज-मजदूरी के काम के लिए सबसे ज्यादा लोग राजस्थान से ही आए। रोजगार की तलाश में, राज-मजदूर ही नहीं, धोबी, नाई चाय-पानवाले और भी तरह-तरह के धंधे करनेवाले
लोग दिल्ली पहुँचने लगे। कहीं नए मकानों की नीवें खोदी जाने लगतीं तो आस-पास के राज-मजदूरों की छोटी-छोटी अनगिनत झोंपड़ियाँ खड़ी हो जातीं, लोहा सीमेंट ईंट-पत्थर के ढेरों के बीच, इन झोंपड़ियों में मोटी-मोटी रोटियाँ सेंकी जाने लगतीं, बच्चे रेत-मिट्टी के ढेरों पर खेलने-सोने लगते, और मजदूरी के काम से निबटकर स्त्रियों की टोलियाँ गाती हुई अपनी-अपनी झोंपड़ियों में लौटने लगतीं। गारे मिट्टी की अधकचरी झोंपड़ियों में भी स्निग्धता आ जाती। पर ज्यों ही पक्के मकानों का मुहल्ला बनकर तैयार हो जाता, तो झोंपड़े वहाँ से उठ जाते, राज-मजदूर हट जाते, जहाँ उनकी झोपड़ियाँ थीं वहाँ सड़क की पटरियाँ बिछ जातीं, आँगनों की दीवारें खिंच जातीं, और पता भी नहीं चल पाता कि कभी वहाँ झोंपड़ियों की पाँते भी रही होंगी।
पर जब रमेश नगर बना, और बनकर तैयार भी हो गया, तो राज-मजदूरों के झोंपड़े ज्यों-के-त्यों बने रहे। कारण, ये झोंपड़े बस्ती से सटकर नहीं बनाए गए थे। इन्हें बस्ती से थोड़ा हटकर बड़ी सड़क के किनारे एक वीरान टीले पर बनाया गया था, जो दो तिरछी सड़को के बीच अलग-अलग-सा खड़ा था। यहाँ पर राज मजदूरों की बस्ती बस गई थी। पहले ढलान के निचले हिस्से में छिपपुट झोंपड़ियाँ बनीं; कोई कहीं, कोई कहीं। फिर धीरे-धीरे झोंपड़ियों के झुरमुट उठ खड़े हुए और
झोंपड़ियाँ जैसे ढलान चढ़ने लगीं। धीरे-धीरे झोंपड़ियों की कतारों के बीच गलियाँ बन गईं। राज-मजदूर अपने भाई-बंदों को भी बुलाने लगे। दिल्ली में चले आओ, शहर बड़ा है। रोजगार का जुगाड़ हो जाएगा, तुम चले आओ। और काम की सचमुच कमी नहीं थी। रमेश नगर बनकर खड़ा हो गया तो उसी की बगल में दक्षिणी रमेश नगर बनने लगा, और वह भी बन चुका तो पश्चिमी रमेश नगर की बारी आ गई। ये तीनों बन चुके तो इनके पीछे पांडव नगर बनने लगा। बस्तियाँ एक पर एक बनती ही जातीं, शहर फैलता ही जाता। फिर यही झोंपड़े पक्के होने लगे। आखिर राज-मजदूर ही तो यहाँ रहते थे,
उनके लिए कच्ची दीवार की जगह ईंटों का फर्श बाँधना क्या मुश्किल था। इस तरह राज-मजदूर अपनी छोटी-सी बस्ती में बने रहे। उनकी औरतें मजदूरी छोड़ रमेश नगर के घरों में ही चौका बर्तन करने लगीं, उनके मर्द और भाई-बंद बसों में बैठकर जगह-जगह इमारती काम पर जाने लगे, और इस तरह दिल्ली के ही बाशिंदे बनकर रहे गए। इनकी अपनी छोटी-सी नगरी बस गई। कभी शाम सवेरे, किसी वक्त इस नगरी में जाओ तो लगता जैसे राजस्थान के ही किसी कस्बे में पहुँच गए हों। रंग-बिरंगे घाघरे, पाँवों में छनकती पाजेब, चारों ओर राजस्थानी रंग छिटके रहते, झोंपड़ों की दीवारों पर राजस्थानी चलन के ही अनुसार, कहीं मोर, तो कहीं हाथी तो कहीं सरपट दौड़ते चेतक घोड़े के चित्र बने रहते। यहीं पर
शादियाँ-ब्याह होने लगे, यहीं पर राज-मजदूरों ने अपनी पंचायतें बना लीं। जहाँ गलियाँ कच्ची थीं, वहाँ धीरे-धीरे चौके बिछ गए, पक्की गलियाँ बन गई। पानी का बड़ा पाइप इधर से ही होकर जाता था, इसलिए कह सुनकर तीन जगह पर नल भी लग गए। चाय-पानी की, सौदा-सूत की छोटी-छोटी दूकानें भी खुल गईं। गोबिंदी का पति जब किसी छत पर काम करते गिरकर मर गया तो पंचायतवालों ने ही उसे चाय की दूकान खोल दी। पक्की कोठरियों के साथ-साथ एक-दूसरे को बाँधने वाले सूत्र और तंतु भी पक्के होने लगे। दो-दो पीढ़ियाँ बस्ती में उम्र लाँघने लगीं। ऐसे छोकरे-छोकरियाँ जिन्होंने राजस्थान की धरती को कभी देखा नहीं था, बस्ती और बस्ती के बाहर रमेश नगर की सड़कों पर घूमती-दौड़ती फिरतीं।
लड़कियाँ बिंदी-लिपस्टिक लगातीं, फोटो खिंचवातीं और शहर में टेलीविजन आ जाने पर शाम को किसी न किसी घर की खिड़की में झाँक-झाँककर टेलीविजन देखतीं। उनकी बस्ती में रेडियो और ट्रांजिस्टरों पर फिल्मी गाने गूँजते। नई पौध को दिल्ली की हवा लगने लगी थी। कोई फिल्म न थी जिसे ये नहीं देखते, कोई फिल्मी गीत नहीं था जिसे ये नहीं गुनगुनाते। कहीं-कहीं पर तो नए-नए गुल भी खिलने लगे थे। साहू की बेटी, राधा, दो बच्चों की माँ, बाहर किसी बस-कंडक्टर के साथ भाग गई। लौंडे-लपाड़ों को शराब-जुआ और आवारागर्दी की लत पड़ने लगी। गोबिंदी की चाय की दूकान पर बस्ती के बड़े-बूढ़े बैठते तो यही चर्चा रहती कि कैसे लौंडे-लौंडियों की खींच-तानकर रखा जाए।
राजस्थानियों की ही इस बस्ती में, सड़क के पास हरयाणा और उत्तरप्रदेश के कुछ नाई, मोची धोबी आदि भी आकर बस गए थे। जात-पात अलग होने के कारण इनके साथ शादी ब्याह के रिश्ते तो नहीं थे, लेकिन उठना-बैठना, दोस्ती-मुरव्वती थोड़ी-बहुत जरूर चलने लगी थी। चौधरी नाई का झोंपड़ा पहले ढलान के नीचे हुआ करता था, फिर एक बुढ़िया के मरने पर वह बस्ती के बीचोबीच उस बुढ़िया के झोंपड़े में आ गया था। काम-काज के लिए यह इसी बस्ती के बाहर सड़क किनारे अपनी नाई की कुर्सी लगाता था। इस तरह, बरसों तक यहीं रहने के कारण वह बहुत कुछ बस्ती के ही जीवन का अंग बन चुका था।
चाय की दूकान में से निकलकर चौधरी ने कदम बढ़ा दिए और तेज-तेज चलता हुआ ढलान उतरने लगा। अभी कुछ कर लो तो कर लो, पीछे कुछ नहीं होगा वह बुदबुदाया और लंबे-लंबे डग भरने लगा। उसकी छोटी-छोटी आँखों में उत्तेजना आ गई थी। ऊँचे-लंबे कद का साँवला-सा आदमी, नीली कमीज में, कंधे झुकाए चलता हुआ भालू-सा लग रहा था।
हवा में ठंडक बढ़ गई थी। अब बारिश की फुहार-सी पड़ने लगी थी। लगता, धुंध में से ही फुहार के कण बन-बनकर मुँह पर लगने लगे हैं। हलके-हलके कण, नुकीले काँटों की तरह मुँह और हाथों को चुभ रहे थे। धुँध छटने लगी थी, ठण्डी हवा के हल्के-हल्के झोंकों से जैसे छन-छनकर बिखर रही थी।
बस्ती की गलियों में चहल-पहल बढ़ गई थी। वातावरण साफ होने लगा था। गलियों में फिर से रंगीनी छिटकने लगी थी। मर्द लोग काम पर देर से जाते थे, औरतें जगह-जगह चौका-बर्तन करने के लिए, पहले से निकल जाती थीं। कोठरियों के बाहर जगह-जगह चूल्हे जलने लगे थे, और काम पर जानेवाले मर्दों के लिए रोटियाँ सेंकी जाने लगी थीं।
अपनी कोठरी के पास से गुजरते हुए चौधरी ने देखा कि उसकी अधेड़ उम्र की पत्नी, रोज की तरह मैली कुचैली बनी, कोठरी के बाहर आग जलाने के लिए चूल्हे में फूँकें मार रही है। अपने पति को पास से गुजरते देख, अपना पोपला मुँह फुलाकर बोली, देर कर दी, आज काम पर नहीं जाओगे ?" चौधरी ने चलते-चलते ही जवाब दिया, "एक मौसम में तेरा बाप हजामत बनवाने आएगा ? ऊपर देखती नहीं, कैसी घटा छाई है ?"
"चाय तो पी जाओ, बनाऊँ ?" उसकी पत्नी ने कहा, जिस पर चौधरी ने चिल्लाकर कहा, बसंती को जगा दे। सुनती है ? मैंने क्या कहा, बसंती को जगा दे, मुँह-हाथ धुला दे। मैं अभी आ रहा हूँ।..."
चौधरी सीधा चलता हुआ, ढलान के नीचे, लँगड़े दर्जी की दूकान पर जा पहुँचा। लँगड़ा दर्जी बुलाकीराम, अपनी दूकान खोले, दूकान के ही बाहर, एक हाथ कमर पर रखे, उचक-उचककर झाड़ू लगा रहा था। दूकान के चबूतरे के ऊपर ऊँची अलगनी पर, स्त्रियों के सिले कपड़े घाघरे अँगियाँ, बच्चों के कुर्ते पाजामे टोपियाँ आदि लटक रहे थे।
"बुलाकीराम, काम शुरू कर दिया, तड़के तड़के ?"
"आओ चौधरी, आओ।" बुलाकी ने कमर सीधी करते हुए कहा, "आओ बैठो, आज सुबह सवेरे दरसन दिए।" और बड़ी फुर्ती से चबूतरे पर से पीढ़ा उठाकर चौधरी के सामने रख दिया। "हमारी अमानत कब मिलेगी ?" बुलाकी छूटते ही बोला।
"तेरी अमानत धरी है, जब ले ले। भले ही आज ही ले ले।" चौधरी ने अपनी छोटी-छोटी आँखें बुलाकी के चेहरे पर गाड़ते हुए जवाब दिया।
इस पर लँगड़े बुलाकी का सारा शरीर पुलक उठा और एक अजीब-सी अस्फुट आवाज उसके कंठ से निकली।
"पहलेवाली बात तो नहीं होगी ना, चौधरी हम बारात सजाकर ले गए और तेरी लौंडिया ने जहर फाँक लिया।"
"अबकी बारात का लफड़ा ही नहीं करेंगे, चुपचाप काम निबटा देंगे।"
"तू अपना घर पक्का कर चौधरी हम तो अपनी लच्छमी के लिए पलकें बिछाए बैठे हैं।" और बुलाकी के कंठ से फिर वही विचित्र-सी आवाज निकली।
"बाहर सौ होंगे। चाहे तो आज ही ब्याह कर ले।" दर्जी के चेहरे की ओर इकटक देखते हुए चौधरी ने स्थिर निश्चेष्ट आवाज में कहा।
"हैं ? क्यों भला ? आठ सौ पर बात पक्की कर चुका है। छः सौ पेशगी ले भी चुका है। अब बारह सौ कह रहा है ? अपनी जबान से मुकर रहा है। यह बात अच्छी नहीं, चौधरी, आदमी को जबान का पक्का होना चाहिए।..."
"बारह सौ होंगे। कहेगा तो आज ही उसके हाथ पीले कर दूँगा। चार सौ पेशगी अभी दे दे, पूरे एक हजार हो जाएँगे, दो सौ, लुगाई घर आ जाने पर दे देना।"
"बारह सौ क्यों ? किस बात के बारह सौ ? आठ सौ पर तैने जबान की थी।"
शुरू हो गया था। बगलवाली कोठरी में से बिसेसर की पत्नी जमुना, सिर पर घड़ा रखे नल पर से पानी लेने के लिए निकली और ढलान चढ़ने लगी। ऊपर बड़े नल के ही पास, ढलान के सिरे पर गोबिंदी की चाय पानी की दूकान खुल गई थी, घनी धुँघ में से भी उसकी बत्ती की लौ नजर आ रही थी। चौधरी ने घूमकर, ढलान के नीचे नजर दौड़ाई। ऊबड़-खाबड़ गली के दोनों ओर खड़ी छोटी-छोटी कोठरियों में भी हरकत शुरू हो गई थी। किसी-किसी कोठरी के बाहर चूल्हा जलने लगा था। कहीं-कहीं बस्ती की कोई लड़की, चादर में मुँह सिर लपेटे, ढलान उतरती हुई, बस्ती के बाहर लोगों के घरों में चौका बर्तन करने जा रही थी। बाहर की बड़ी सड़क अभी से चलने लगी थी, दूर से लारियों-मोटरों के भोंपुओं की आवाजें, धुंध और कोहरे में लिपटी-सी सुनाई पड़ने लगी थीं।
हर बार, बारिश का समा होने पर चौधरी बड़बड़ाता था। आज तो धुंध भी थी और बादल भी घिरे थे जो न जाने कब बरसने लगें। आज तो अपने अड्डे पर जाने में कोई तुक नहीं, कौन इस मौसम में बाल कटवाने या हजामत बनवाने आएगा। आज का दिन भी बर्बाद गया समझो। उसका मन हुआ, बैठकर बीड़ी सुलगा ले। उसने अपने नीले कुर्ते की जेब से बीड़ी निकाली भी, पर फिर अपनी ही कोठरी के बाहर बैठने के बजाए बाहर निकल आया और गोबिंदी की चाय की दूकान की ओर कदम बढ़ा दिए। कल हीरा और धन्ना और बस्ती के कुछ और लोग हकीम से मिलने गए थे, दिन-भर बाहर बने रहे, कुछ पता तो चले, स्याह-सफेद क्या कर आए हैं। सरकार ने क्या कहा है, क्या फैसला दिया है। सुबह सवेरे, हर रोज, अपने-अपने काम पर जाने से पहले, कुछ देर के लिए, गोबिंदी की दूकान में छोटा-मोटा जमाव जरूर होता था। कुछ लोग तो जरूर वहाँ बैठे होंगे।
जब चौधरी गोबिंदी के चाय-घर के पास पहुँचा तो सचमुच वहाँ जमाव था, और दूर से ही हीरा की आवाज सुनाई पड़ रही थी, ऊँची आवाज में बोल रहा था, ‘‘हमने हाथ बाँधकर कहा, ‘‘मालिक हम राज-मिस्त्री हम ही घर बनावैं और हमारे ही रहने को ठौर नहीं, लोगों को घर जुटावैं और अपना सिर छिपाने के लिए जगह ही नहीं। इस मेंह-बरसात में तो हमें बेघर नहीं करो।’’
‘‘फिर हाकिम क्या बोला ?’’ किसी की आवाज आई। ‘‘हाकिम भला लोग था। बड़े धीरज से बात सुनता रहा। बड़े अफसर तो भले लोग ही होते हैं, हरामी तो नीचेवाले छोटे अफसर होते हैं।’’...हीरा कह रहा था।
तभी चौधरी ने चाय घर में कदम रखा।
‘‘क्या कर आए हो, हीरा ? हाकिम लोग मान गए ?’’ कहते हुए चौधरी चबूतरे पर बैठ गया। चाय घर में बस्ती के सात-आठ आदमी बैठ थे। हीरा अभी भी सिर पर राजस्थानी पग्गड़ बाँधे और कलवाले ही उजले कपड़े और काली बास्कट पहने था जिन्हें पहनकर वहा हाकिमों से मिलने गया था।
चौधरी के अंदर आ जाने पर भी चाय घर में बैठे लोगों ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। बरसों से इस बस्ती के छोर पर रहने के बावजूद उसे अभी भी बाहर का, छोटी जात का आदमी ही माना जाता था। चौधरी अहीर था जबकि ये लोग राजस्थानी थे। फिर वह नौवा, और ये राज-मजदूर राज-मिस्त्री। वह अपनी जात-बिरादरी से कटा हुआ—बस्ती में तीन-चार ही घर अहीरों के थे, और वे भी एक-दूसरे से फटे हुए—जबकि इन लोगों की पूरी बिरादरी थी,
अपनी पंचायत थी, ये लोग आपस में गठे हुए थे। चौधरी के सवाल की तरफ विशेष ध्यान न देते हुए, हीरा मिस्त्री कहे जा रहा था, ‘‘बात तो तब बिगड़ी जब बड़े साहिब ने हमें छोटे अफसर के सुपुर्द कर दिया, कि इनसे बात करो, यह तुम्हें सब बात समझा देंगे। बस, तभी बात बिगड़ी। सच पूछो, तो जब यह छोटा अफसर अंदर घुसा तो मेरे अंदर से आवाज आई हीरा, मामला बिगड़ गया है। मालिक ने जैसे गाय की रस्सी अपने हाथों से कसाई के हाथ में दे दी हो। अंदर से ही जैसे फुरनी फुरती है, मुझे पता चला गया कि मामला बिगड़ गया है।’’
‘‘क्यों ?’’
‘‘क्यों क्या ? छोटे अफसर ने हमें बोलने ही नहीं दिया-हमें अपने दफ्तर में ले गया और फैसला सुना दिया-तुम्हें निकलना होगा, बस्ती खड़ी नहीं रह सकती। पूछो रामपरकाश से। इसने कुछ कहने को मुँह खोला कि वह अफसर कड़ककर बोला, सरकार ने जो फैसला करना था, कर दिया। अब बहस करने की कोई जरूरत नहीं।’ लो सुनो, यह भी कोई बोलने का ढंग है। अरे बोलो तो मीठा, काम तो होगा,
नहीं होगा, यह तो भगवान के हाथ है, पर बोलो तो मीठा। हमसे कड़वा बोलकर तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारे भाग अच्छे थे, तुम अफसर बन गए। हमारे भाग खोटे थे, हम मिस्त्री-मजूर बने, पर भाई बोलो तो मीठा। हमारा पानी तो नहीं उतारो हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं, हमारी पगड़ी तो न हीं उछालो। हमारे बाप-दादा भी जमीन-जायदादवाले थे, अभी भी राजस्थान में हमारी अपनी खेती है। अब वहाँ सूखा पड़े तो हम क्या करें ? बाल-बच्चों का पेट पालने के लिए दिल्ली चले आए। पर हमारे साथ बोलो तो मीठा !’’
किसी गीत की स्थायी पंक्ति की भाँति हीरा बार-बार यही वाक्य दोहराए जा रहा था-बोलो तो मीठा, भाई हमारे साथ बोलो तो मीठा !
चौधरी समझ गया कि मामला बिगड़ गया है। पिछले दिन, बस्ती के तीन और लोगों को साथ लेकर हीरा ‘सरकार’ से मिलने गया था। पूरा राजस्थानी बाना पहनकर तीनों जने गए थे। सिर पर पग्गड़ आँखों में काजल घेरेदार ‘अँगरखा’ और तेल-चिपुड़ी लाठी हरेक के हाथ में थी। चौधरी ने ही तीनों की हजामत भी बनाई थी, और चलते समय हँसी-हँसी में कहा भी था, ‘‘अब काजल सुरमा लगाकर चले हो तो काम निबटाकर लौटना।
पहले की तरह खाली हाथ नहीं लौट आना। पर उधर अफसर ने बिना बात सुने चलता कर दिया था और धमकी दी थी कि चपरासी को बुलाकर बाहर निकाल देगा।
‘‘हाकिम अच्छा मिल जाए, यह भी किस्मत की बात होती है। पिछली बार जब बस्ती तोड़ने की बात चली थी, तो हम जिस साहिब से मिले थे, वह तो घंटे तक हमारी बात सुनता रहा और मामला आगे नहीं बढ़ने दिया था।’’
‘‘तुम कल भी उसी अफसर से जा मिलते, उसके सामने हाथ जोड़ते।’’
‘‘यही तो कहा, किस्मत खोटी हो तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। उसी के दफ्तर में तो गए थे। पर वह अब वहाँ पर नहीं बैठता। किसी दूसरे दफ्तर में काम करता है। उससे मेल-मुलाकात हो जाती तो जरूर कोई रास्ता निकल आता।’’
‘‘अब क्या कर आए हो ?’’
‘‘हम क्या करेंगे ? हाथ बाँधकर गए थे, हाथ बाँधकर ही लौट आए।’’
‘‘वह नहीं तो किसी दूसरे अफसर से मिलो। किसी मंतरीजी सेमिलो।’’
इस पर मूलराज बोला, ‘‘हमने पहले ही कहा था, पक्के घर यहाँ नहीं बनाओ, न तुम्हारी जमीन, न तुम्हारे नाम का पट्टा।’’
"दस-बीस रोज की बात होती तो कच्ची झोंपड़ियों में पड़े रहते। अब तो यहाँ रहते भी बरसों बीत गए। घर पक्का बना लिया तो क्या गुनाह किया।"
मूलराज लोहे की कुर्सी के ऊपर दोनों पाँव चढ़ाए बैठा था, और बीड़ी के कश ले रहा था। कल रोज घिरे बादलों के बावजूद वह एक घर में पुताई का काम करता रहा था, और पुताई के छींटे अभी भी उसके हाथों और पाँवों पर पड़े थे। एकाध छींटा उसके मुँह पर भी मौजूद था।
"तो क्या कहते हो, आज काम पर नहीं जाएँ ?"
"नहीं, काम पर क्यों नहीं जाएँ। यह काम इतनी जल्दी थोड़े ही निबटते हैं। हमें यहाँ से निकालेंगे भी तो महीना-दो महीना तो लग ही जाएगा। अभी कागज ऊपर जाएँगे।"
"यह पहली बार तो बस्ती गिराने की बात नहीं हुई ना, कई बार पहले भी हो चुकी है। क्या मालूम अबकी बार भी बस्ती बच जाए। हाकिम के दिल की कौन जाने।"
"उन्होंने महीने-भर का नोटिस दिया था, वह तो खत्म हो गया।" चौधरी ने अपनी छोटी-छोटी शंकित आँखों से देखते हुए कहा।
"नोटिस की बात नहीं करो, वे तो आए दिन मिलते रहते हैं।"
खौलती चाय की केतली के पास बैठी गोबिंदी बोली, "तुम मर्द लोग डरते काँपते ही रहोगे। अबकी बार अफसर से मिलने जाओ तो मुझे साथ ले चलना। अफसर को ऐसी फटकार सुनाऊँगी कि नानी याद करा दूँगी।"
"तू क्या कहेगी, रानी ?"
"मैं कहूँगी, जिस जमीन पर हमारी कोठरियाँ खड़ी हैं, वे हमारे नाम कर दो। और हमसे जमीन के पैसे ले लो। कोठरियाँ तो हमने अपने पैसों से बनाई हैं, इन्हें कोई क्यों तोड़े ? हमारा नुकसान भी करें और हमें बेघर भी करें। तुम्हारे मुँह से बात ही नहीं निकलती। अँगरखे पहने कचहरी में मटक-मटककर आ गए।"
"कहती तो ठीक हो", मूलराज ने कहा, "हीरा, हमें यही कहना चाहिए था।"
"अरे, कोई बात सुने तब ना। पहले यह नहीं कहा था ? यही तो बरसों से कहते आ रहे हैं। कोई सुने तो। हम एक नहीं, दस तरकीबें बतावैं। हम अनाड़ी तो नहीं हैं, हमारे हाथ से बीसियों घर बने हैं।"
"आज फिर चले चलो, गोबिंदी को भी ले चलो। क्यों हीरा ? तुमने तो अभी अपने वस्तर भी नहीं उतारे।" चौधरी ने मसखरी करते हुए कहा।
हीरा ने हल्के-से सिर हिलाया, "कोई अच्छा अफसर मिल जाए तो बात बन जाए।"
चौधरी चुपचाप चबूतरे पर से उठकर बाहर आ गया।
बस्ती क्या थी, दिल्ली की ही एक सड़क के किनारे छोटा सा राजस्थान बना हुआ था। आजादी के बाद, दिल्ली शहर फैलने लगा था। नई-नई बस्तियों की उसारी होने लगी थी और उन बस्तियों को बनाने के लिए जगह-जगह से राज-मजदूर खिंचे आने लगे थे। दिल्ली से दूर, जहाँ कहीं सूखा पड़ता या बाढ़ आती, वहीं से लोग उठ-उठकर दिल्ली की ओर भागने लगते। कहीं परिवार के परिवार चले आए, कहीं अकेले मर्द कहीं छोटी उम्र के लौंडे लड़के भी। कहीं राजस्थान से तो कहीं हरयाणा और पंजाब के गाँवों से, और कहीं तो दूर दक्षिण से भी; पर राज-मजदूरी के काम के लिए सबसे ज्यादा लोग राजस्थान से ही आए। रोजगार की तलाश में, राज-मजदूर ही नहीं, धोबी, नाई चाय-पानवाले और भी तरह-तरह के धंधे करनेवाले
लोग दिल्ली पहुँचने लगे। कहीं नए मकानों की नीवें खोदी जाने लगतीं तो आस-पास के राज-मजदूरों की छोटी-छोटी अनगिनत झोंपड़ियाँ खड़ी हो जातीं, लोहा सीमेंट ईंट-पत्थर के ढेरों के बीच, इन झोंपड़ियों में मोटी-मोटी रोटियाँ सेंकी जाने लगतीं, बच्चे रेत-मिट्टी के ढेरों पर खेलने-सोने लगते, और मजदूरी के काम से निबटकर स्त्रियों की टोलियाँ गाती हुई अपनी-अपनी झोंपड़ियों में लौटने लगतीं। गारे मिट्टी की अधकचरी झोंपड़ियों में भी स्निग्धता आ जाती। पर ज्यों ही पक्के मकानों का मुहल्ला बनकर तैयार हो जाता, तो झोंपड़े वहाँ से उठ जाते, राज-मजदूर हट जाते, जहाँ उनकी झोपड़ियाँ थीं वहाँ सड़क की पटरियाँ बिछ जातीं, आँगनों की दीवारें खिंच जातीं, और पता भी नहीं चल पाता कि कभी वहाँ झोंपड़ियों की पाँते भी रही होंगी।
पर जब रमेश नगर बना, और बनकर तैयार भी हो गया, तो राज-मजदूरों के झोंपड़े ज्यों-के-त्यों बने रहे। कारण, ये झोंपड़े बस्ती से सटकर नहीं बनाए गए थे। इन्हें बस्ती से थोड़ा हटकर बड़ी सड़क के किनारे एक वीरान टीले पर बनाया गया था, जो दो तिरछी सड़को के बीच अलग-अलग-सा खड़ा था। यहाँ पर राज मजदूरों की बस्ती बस गई थी। पहले ढलान के निचले हिस्से में छिपपुट झोंपड़ियाँ बनीं; कोई कहीं, कोई कहीं। फिर धीरे-धीरे झोंपड़ियों के झुरमुट उठ खड़े हुए और
झोंपड़ियाँ जैसे ढलान चढ़ने लगीं। धीरे-धीरे झोंपड़ियों की कतारों के बीच गलियाँ बन गईं। राज-मजदूर अपने भाई-बंदों को भी बुलाने लगे। दिल्ली में चले आओ, शहर बड़ा है। रोजगार का जुगाड़ हो जाएगा, तुम चले आओ। और काम की सचमुच कमी नहीं थी। रमेश नगर बनकर खड़ा हो गया तो उसी की बगल में दक्षिणी रमेश नगर बनने लगा, और वह भी बन चुका तो पश्चिमी रमेश नगर की बारी आ गई। ये तीनों बन चुके तो इनके पीछे पांडव नगर बनने लगा। बस्तियाँ एक पर एक बनती ही जातीं, शहर फैलता ही जाता। फिर यही झोंपड़े पक्के होने लगे। आखिर राज-मजदूर ही तो यहाँ रहते थे,
उनके लिए कच्ची दीवार की जगह ईंटों का फर्श बाँधना क्या मुश्किल था। इस तरह राज-मजदूर अपनी छोटी-सी बस्ती में बने रहे। उनकी औरतें मजदूरी छोड़ रमेश नगर के घरों में ही चौका बर्तन करने लगीं, उनके मर्द और भाई-बंद बसों में बैठकर जगह-जगह इमारती काम पर जाने लगे, और इस तरह दिल्ली के ही बाशिंदे बनकर रहे गए। इनकी अपनी छोटी-सी नगरी बस गई। कभी शाम सवेरे, किसी वक्त इस नगरी में जाओ तो लगता जैसे राजस्थान के ही किसी कस्बे में पहुँच गए हों। रंग-बिरंगे घाघरे, पाँवों में छनकती पाजेब, चारों ओर राजस्थानी रंग छिटके रहते, झोंपड़ों की दीवारों पर राजस्थानी चलन के ही अनुसार, कहीं मोर, तो कहीं हाथी तो कहीं सरपट दौड़ते चेतक घोड़े के चित्र बने रहते। यहीं पर
शादियाँ-ब्याह होने लगे, यहीं पर राज-मजदूरों ने अपनी पंचायतें बना लीं। जहाँ गलियाँ कच्ची थीं, वहाँ धीरे-धीरे चौके बिछ गए, पक्की गलियाँ बन गई। पानी का बड़ा पाइप इधर से ही होकर जाता था, इसलिए कह सुनकर तीन जगह पर नल भी लग गए। चाय-पानी की, सौदा-सूत की छोटी-छोटी दूकानें भी खुल गईं। गोबिंदी का पति जब किसी छत पर काम करते गिरकर मर गया तो पंचायतवालों ने ही उसे चाय की दूकान खोल दी। पक्की कोठरियों के साथ-साथ एक-दूसरे को बाँधने वाले सूत्र और तंतु भी पक्के होने लगे। दो-दो पीढ़ियाँ बस्ती में उम्र लाँघने लगीं। ऐसे छोकरे-छोकरियाँ जिन्होंने राजस्थान की धरती को कभी देखा नहीं था, बस्ती और बस्ती के बाहर रमेश नगर की सड़कों पर घूमती-दौड़ती फिरतीं।
लड़कियाँ बिंदी-लिपस्टिक लगातीं, फोटो खिंचवातीं और शहर में टेलीविजन आ जाने पर शाम को किसी न किसी घर की खिड़की में झाँक-झाँककर टेलीविजन देखतीं। उनकी बस्ती में रेडियो और ट्रांजिस्टरों पर फिल्मी गाने गूँजते। नई पौध को दिल्ली की हवा लगने लगी थी। कोई फिल्म न थी जिसे ये नहीं देखते, कोई फिल्मी गीत नहीं था जिसे ये नहीं गुनगुनाते। कहीं-कहीं पर तो नए-नए गुल भी खिलने लगे थे। साहू की बेटी, राधा, दो बच्चों की माँ, बाहर किसी बस-कंडक्टर के साथ भाग गई। लौंडे-लपाड़ों को शराब-जुआ और आवारागर्दी की लत पड़ने लगी। गोबिंदी की चाय की दूकान पर बस्ती के बड़े-बूढ़े बैठते तो यही चर्चा रहती कि कैसे लौंडे-लौंडियों की खींच-तानकर रखा जाए।
राजस्थानियों की ही इस बस्ती में, सड़क के पास हरयाणा और उत्तरप्रदेश के कुछ नाई, मोची धोबी आदि भी आकर बस गए थे। जात-पात अलग होने के कारण इनके साथ शादी ब्याह के रिश्ते तो नहीं थे, लेकिन उठना-बैठना, दोस्ती-मुरव्वती थोड़ी-बहुत जरूर चलने लगी थी। चौधरी नाई का झोंपड़ा पहले ढलान के नीचे हुआ करता था, फिर एक बुढ़िया के मरने पर वह बस्ती के बीचोबीच उस बुढ़िया के झोंपड़े में आ गया था। काम-काज के लिए यह इसी बस्ती के बाहर सड़क किनारे अपनी नाई की कुर्सी लगाता था। इस तरह, बरसों तक यहीं रहने के कारण वह बहुत कुछ बस्ती के ही जीवन का अंग बन चुका था।
चाय की दूकान में से निकलकर चौधरी ने कदम बढ़ा दिए और तेज-तेज चलता हुआ ढलान उतरने लगा। अभी कुछ कर लो तो कर लो, पीछे कुछ नहीं होगा वह बुदबुदाया और लंबे-लंबे डग भरने लगा। उसकी छोटी-छोटी आँखों में उत्तेजना आ गई थी। ऊँचे-लंबे कद का साँवला-सा आदमी, नीली कमीज में, कंधे झुकाए चलता हुआ भालू-सा लग रहा था।
हवा में ठंडक बढ़ गई थी। अब बारिश की फुहार-सी पड़ने लगी थी। लगता, धुंध में से ही फुहार के कण बन-बनकर मुँह पर लगने लगे हैं। हलके-हलके कण, नुकीले काँटों की तरह मुँह और हाथों को चुभ रहे थे। धुँध छटने लगी थी, ठण्डी हवा के हल्के-हल्के झोंकों से जैसे छन-छनकर बिखर रही थी।
बस्ती की गलियों में चहल-पहल बढ़ गई थी। वातावरण साफ होने लगा था। गलियों में फिर से रंगीनी छिटकने लगी थी। मर्द लोग काम पर देर से जाते थे, औरतें जगह-जगह चौका-बर्तन करने के लिए, पहले से निकल जाती थीं। कोठरियों के बाहर जगह-जगह चूल्हे जलने लगे थे, और काम पर जानेवाले मर्दों के लिए रोटियाँ सेंकी जाने लगी थीं।
अपनी कोठरी के पास से गुजरते हुए चौधरी ने देखा कि उसकी अधेड़ उम्र की पत्नी, रोज की तरह मैली कुचैली बनी, कोठरी के बाहर आग जलाने के लिए चूल्हे में फूँकें मार रही है। अपने पति को पास से गुजरते देख, अपना पोपला मुँह फुलाकर बोली, देर कर दी, आज काम पर नहीं जाओगे ?" चौधरी ने चलते-चलते ही जवाब दिया, "एक मौसम में तेरा बाप हजामत बनवाने आएगा ? ऊपर देखती नहीं, कैसी घटा छाई है ?"
"चाय तो पी जाओ, बनाऊँ ?" उसकी पत्नी ने कहा, जिस पर चौधरी ने चिल्लाकर कहा, बसंती को जगा दे। सुनती है ? मैंने क्या कहा, बसंती को जगा दे, मुँह-हाथ धुला दे। मैं अभी आ रहा हूँ।..."
चौधरी सीधा चलता हुआ, ढलान के नीचे, लँगड़े दर्जी की दूकान पर जा पहुँचा। लँगड़ा दर्जी बुलाकीराम, अपनी दूकान खोले, दूकान के ही बाहर, एक हाथ कमर पर रखे, उचक-उचककर झाड़ू लगा रहा था। दूकान के चबूतरे के ऊपर ऊँची अलगनी पर, स्त्रियों के सिले कपड़े घाघरे अँगियाँ, बच्चों के कुर्ते पाजामे टोपियाँ आदि लटक रहे थे।
"बुलाकीराम, काम शुरू कर दिया, तड़के तड़के ?"
"आओ चौधरी, आओ।" बुलाकी ने कमर सीधी करते हुए कहा, "आओ बैठो, आज सुबह सवेरे दरसन दिए।" और बड़ी फुर्ती से चबूतरे पर से पीढ़ा उठाकर चौधरी के सामने रख दिया। "हमारी अमानत कब मिलेगी ?" बुलाकी छूटते ही बोला।
"तेरी अमानत धरी है, जब ले ले। भले ही आज ही ले ले।" चौधरी ने अपनी छोटी-छोटी आँखें बुलाकी के चेहरे पर गाड़ते हुए जवाब दिया।
इस पर लँगड़े बुलाकी का सारा शरीर पुलक उठा और एक अजीब-सी अस्फुट आवाज उसके कंठ से निकली।
"पहलेवाली बात तो नहीं होगी ना, चौधरी हम बारात सजाकर ले गए और तेरी लौंडिया ने जहर फाँक लिया।"
"अबकी बारात का लफड़ा ही नहीं करेंगे, चुपचाप काम निबटा देंगे।"
"तू अपना घर पक्का कर चौधरी हम तो अपनी लच्छमी के लिए पलकें बिछाए बैठे हैं।" और बुलाकी के कंठ से फिर वही विचित्र-सी आवाज निकली।
"बाहर सौ होंगे। चाहे तो आज ही ब्याह कर ले।" दर्जी के चेहरे की ओर इकटक देखते हुए चौधरी ने स्थिर निश्चेष्ट आवाज में कहा।
"हैं ? क्यों भला ? आठ सौ पर बात पक्की कर चुका है। छः सौ पेशगी ले भी चुका है। अब बारह सौ कह रहा है ? अपनी जबान से मुकर रहा है। यह बात अच्छी नहीं, चौधरी, आदमी को जबान का पक्का होना चाहिए।..."
"बारह सौ होंगे। कहेगा तो आज ही उसके हाथ पीले कर दूँगा। चार सौ पेशगी अभी दे दे, पूरे एक हजार हो जाएँगे, दो सौ, लुगाई घर आ जाने पर दे देना।"
"बारह सौ क्यों ? किस बात के बारह सौ ? आठ सौ पर तैने जबान की थी।"
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book










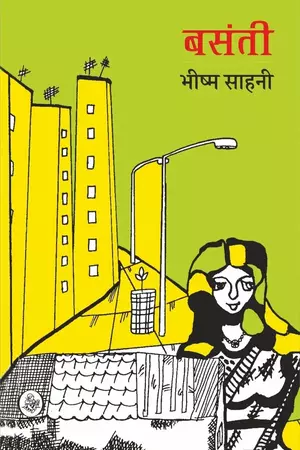

_s.webp)