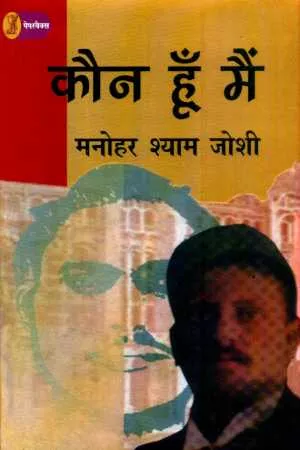|
विविध उपन्यास >> कौन हूँ मैं कौन हूँ मैंमनोहर श्याम जोशी
|
253 पाठक हैं |
|||||||
जोशी की एक महात्त्वाकांक्षी औपन्यासिक कृति...
Kalpana Chakma
प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश
‘कौन हूँ मैं’ जोशी की ऐसी महात्त्वाकांक्षी औपन्यासिक कृति है। जिसे वह प्रकाशित रूप में नहीं देख सके। अपने आखिरी दिनों में वे इस उपन्यास को पूरा करने में लगे थे। लाजवाब किस्सागोई के साथ अचूक व्यंग्यात्मकता जोशी जी के लेखन की विशेषता रही है। उनके इस नवीनतम उपन्यास में किस्सागोसाई का जादू तो है, पर जिसे कहते हैं व्यंग्यात्मकता वह दुनिया के पेच-ओ-खम में उलझे उपन्यास के नायक के जीवन में इस तरह आती है कि सिर्फ हँसने से काम नहीं चलता।
यहाँ एक विराट विडम्बना से साक्षात्कार होता है, जो नायक को जिन्दगी के ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ उसे पूरी दुनिया मृत मान चुकी है और उसे अपने जीवित होने को सिद्ध करने के लिए अन्ततः न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। ब्रिटिशकालीन बंगाल में अवस्थित कथा, भवाल राजपरिवार के मजोकुमार की अविश्वसनीय कथा, मृत्यु के बाद जिसका शव चिता से गायब हो गया और बरसों बाद जब एक साधु ने खुद के मजोकुमार होने का दावा किया तब सम्पत्ति और सम्बन्धों के ताने-बाने में उलझी एक ऐसी गाथा का उद्धाटन हुआ जिसने पूरे देश को रोमांचित कर दिया।
यहाँ एक विराट विडम्बना से साक्षात्कार होता है, जो नायक को जिन्दगी के ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ उसे पूरी दुनिया मृत मान चुकी है और उसे अपने जीवित होने को सिद्ध करने के लिए अन्ततः न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। ब्रिटिशकालीन बंगाल में अवस्थित कथा, भवाल राजपरिवार के मजोकुमार की अविश्वसनीय कथा, मृत्यु के बाद जिसका शव चिता से गायब हो गया और बरसों बाद जब एक साधु ने खुद के मजोकुमार होने का दावा किया तब सम्पत्ति और सम्बन्धों के ताने-बाने में उलझी एक ऐसी गाथा का उद्धाटन हुआ जिसने पूरे देश को रोमांचित कर दिया।
प्राक्कथन
के ? आमि
इसे प्रभु की कृपा कहिए पाठकगण कि दैनन्दिन्य व्यापारों में निहित गूढ़ दार्शनिक वैधानिक प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित ही नहीं होता, अन्यथा पगला जाते हम सब। अब जैसे यही लीजिए ना कि बाहर से किसी के साँकल से द्वार के पट खटखटाने पर भीतर से कोई जिज्ञासा करता है, ‘के’ ? और बाहरवाला उत्तर देता है ‘आमि।’ प्रश्न : कौन ?, उत्तर : मैं। कभी-कभी भीतरवाला बाहरवाले को मात्र वाणी के आधार पर पहचान कर पट खोल देता है। सर्वनाम ही पर्याप्त होता है उस सहजविश्वासी के लिए। वह सोचता ही नहीं कि कहीं कोई ठग, अपना स्वर बदलकर न बोल रहा हो। किन्तु सामान्यतः केवल ‘आमि’ कह देने मात्र से काम नहीं चलता। परिभाषित और परिसीमित करना होता है उस ‘मैं’ को। सर्वप्रथम सर्वनाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके-आमि निरंजन। निरंजन भी अनेक हैं इस सृष्टि में अस्तु, इससे आगे जातिवाचक संज्ञाओं की शरण ली जाती है। मैं निरंजन भट्टाचार्या आपके जमाई बाबू का भांजा।
बहुधा इतना पर्याप्त होता है पट खोल दिए जाने के लिए। किन्तु यदि भीतर वाला स्वभाव से शंकालु हो अथवा इधर जाली परिचय देकर द्वार खुलवा लेने और लूटकर चले जाने की कुछ घटनाएँ चर्चा में रही हों तो सम्भव है कि पट बन्द ही रहें। उत्तर चाहे तो भीतरवाले के अविश्वास को निर्मूल सिद्ध करने का यत्न करते रह सकता है। किन्तु वह अविश्वास और आशंका निर्मूल नहीं। इस असार संसार में पग-पग पर धोखे हैं। बोलबाला है ठग विद्या का। कोई लुटेरा-हत्यारा कहीं से यह पूछकर आ गया हो सकता है कि गृहस्वामी के जमाई बाबू के भांजे का नाम निरंजन भट्टाचार्या है। पछताने से अच्छा है पछतावे की नौबत ही न आने देना। यदि आगंतुक वास्तव में जमाई बाबू का भांजा ही सिद्ध हो तो उससे और जमाई बाबू से क्षमा-याचना की जा सकती है बाद में। बुद्धिमत्ता इसी मैं है कि जो ‘के’ के उत्तर में ‘आमि’ कह रहा हो उसका ‘आमि’ को परिभाषित और परिसीमित कर देना अपर्याप्त माना जाए। उससे यह प्रमाणित करने को कहा जाए कि उस परिभाषा और परिसीमन से जो व्यक्ति निरूपित होता है वह सचमुच उसकी काया में बसता है। सभी सरकारी व्यापारों में पहचानपत्रों, हलफनामों हस्ताक्षरों, अंगूठा-निशानों को यूँ ही तो अनिवार्य नहीं बना दिया गया है ना।
तो पाठकगण आप उस बन्द द्वार की साँकल की ओर हाथ बढ़ाते हुए एक क्षण ठिठकर सोच लिया करें कि चुनौती मिलने की स्थिति में आप अपने ‘आमि’ को प्रमाणित कर सकने की किसी युक्ति से लैस हैं कि नहीं ? यथा मैं वही निरंजन हूँ जिसने मामा के यहाँ आपका बनाया हुआ कटहल का अचार इतने स्वाद से खाया था कि मामी-माँ अगली बार मायके से लौटीं तो एक अमृतबान मेरे लिए भी भरवा लाईं उसका। और यदि इस पर भी द्वार न खुले तो यह कि मैं तो आपको आपके जमाई बाबू का एक पत्र देने आया था। चलिए द्वार के नीचे से सरका देता हूँ, नमस्कार। इधर पत्र खोलकर हस्ताक्षर देखे जमाई बाबू के कि उधर द्वार खोलकर आपको पुकार लिया जाएगा क्षमा-याचनाओं की झड़ी लगाते हुए। यों यदि द्वार के उस पार का व्यक्ति छाछ को भी फूँक-फूँककर पीने के लिए बाध्य कर दिया जा चुका हो तो वह यह सोचकर द्वार न खोलना ही उचित समझा जाता है कि कटहल के अचार वाला प्रसंग किसी और को भी पता हो सकता है तथा जाली हस्ताक्षरों के केस तो प्रायः होते ही रहते हैं। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि हर व्यक्ति को तब तक जाली ही समझा जाए जब तक कि वह अपना असली होना प्रमाणित न कर दे और इसके साथ ही इस बात को कदापि न भुलाया जाए कि प्रमाण भी जाली, भ्रामक और झूठे हो सकते हैं। मेरे गुरु बाबा धर्मदास कहा करते थे कि महाठगिनी माया का जाल है यह संसार और इसमें सब कुछ जाली और झूठा है।
विश्वास मानिए पाठकगण कि जब-जब आप किसी शंकालु के घर के बन्द द्वार की साँकल की ओर हाथ बढ़ा रहे होंगे तब-तब मेरी सहानुभूति आप पर पंखा झल रही होगी। मैं तो आपसे कहीं अधिक दयनीय स्थिति में हूँ। आप जब अपने घर का द्वार खटखटाते हैं तब भीतर से पत्नी द्वारा पूछे गए ‘के ?’ के उत्तर में आपका ‘आमि’ कह देना न केवल पर्याप्त रहता होगा वरन् आप भीतर चरण रखते हुए यह टिप्पणी करने को स्वतंत्र मानते होंगे अपने को कि क्यों व्यर्थ के प्रश्न करती हो, इस वेला और कौन आता है यहाँ ? किन्तु यदि कहीं मेरे और उस स्त्री के मध्य कोई बन्द द्वार हो जिससे मैं सात फेरे लेकर बँधा हुआ हूँ तो साँकल की ओर बढ़ते मेरे हाथ यह सोचकर ठिठक जाएँगे कि उसकी ‘के?’ के उत्तर में अपने ‘आमि’ को किस प्रकार परिभाषित करना उचित होगा मेरे लिए ? यदि यह कहूँ कि तुम्हारा स्वामी हूँ तो वह क्यों खोलेगी भला जबकि सार्वजनिक रूप से घोषित कर चुकी है कि मेरे पति का देहान्त हो चुका है ? द्वार खोलकर एक ठो भूत को कौन स्त्री अपना भविष्य बनाना चाहेगी, बोलिए तो। और यदि मैं यह कहूँ कि मैं वह ठग हूँ जो अपने को तुम्हारा पति बताता घूम रहा है तो वह पुलिस को ही बुलाएगी ना। शासकीय निषेध है मेरे उस भद्र महिला की बाड़ी के आस-पास जाने पर।
आमि-आमि का सतत जाप करते पाठकगण सावधान। आप तभी तक आप हैं जब तक दूसरे आपको आप मान रहे हैं। और सकल व्यापार में चिन्ता करते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे किन्तु इस विषय में कभी चिन्तित नहीं होते कि लोग आप को आप नहीं कहेंगे तब क्या गति होगी आपकी ? कल्पना कीजिए मैं यह गाथा लिख नहीं रहा हूँ, सुना रहा हूँ आपको वैसे ही एक विराट मैदान में जिसमें जयदेवपुर की राजबाड़ी का पोलो ग्राउण्ड था। मैं आपमें से एक की ओर तर्जनी उठाकर जिज्ञासा करता हूँ, ‘आपनि के ?’ और वह एक उत्तर देता है, ‘आमि निरोंजोन भट्टाचार्ज्या।’ और तभी क्या होता है कि आपमें से कुछ हँसकर और कुछ क्रुद्ध होकर सूचित करते हैं मुझे कि यह निरंजन भट्टाचार्ज्या नहीं हैं। मैं उस व्यक्ति को पागल अथवा ठग मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाऊँगा क्या ? पागल तो अपने को कुछ भी मान लेते हैं। जयदेवपुर के पगले दीपेन बाबू तो अपने को क्वीन विक्टोरिया कहते डोलते थे। ठगों का तो काम ही किसी अन्य की अस्मिता ओढ़ लेना है। अब कल्पना कीजिए कि वह श्रोता-विशेष न ठग था, न पागल। वह तो वास्तव में जन्मजात निरंजन भट्टाचार्ज्या ही था किन्तु अन्य लोगों ने किसी कारणवश उसकी अस्मिता निरस्त कर डालने का एक विराट षड्यन्त्र रच रखा था। ऐसे में वह मेरे लिए या किसी के लिए भी निरंजन भट्टाचार्ज्या रह सकता था भला ? उस एक अकेले की बात उन अन्य हजारों की बात के आगे ठहर सकती है भला ? अकाट्य होता है संख्या का तर्क। तो निरंजन भट्टाचार्ज्या आप सभी पाठकगण प्रभु का धन्यवाद करते रहें कि आपको निरोंजोन भट्टाचार्ज्या आमि ही मान रहे हैं सब जन। कहीं यह नहीं कहा जा रहा है कि आप बंगभूमि के छेले न होकर पंजाब दे पुत्तर निरंजन सिंह हैं। और जाल अर्थात् जाली निरोंजोन भट्टाचार्ज्या बने घूम रहे हैं।
कृपया यह न समझें कि मैं अपनी पत्नी पर यह आक्षेप लगाना चाहता हूँ कि उसने मेरी अस्मिता की व्यापक अस्वीकृति के लिए कोई विराट षड्यन्त्र रचा है। वस्तुस्थिति तो यह है कि वह ऐसा समझती है या उसे समझा दिया गया है कि कुछ स्वार्थी लोगों ने एक ठो अपात्र पर मेरे दिवंगत पति की अस्मिता आरोपित कर देने का विराट षड्यन्त्र रचा है। उस बेचारी के मन में ऐसी आशंका उठना स्वाभाविक है। और पाठकगण जब आप का आप होना दूसरों के आप को आप मानने पर निर्भर है अंततः तब संख्या का तर्क जैसे असली निरंजन भट्टाचार्ज्या को जाली सिद्ध कर सकता है तब जाली निरंजन भट्टाचार्ज्या को असली क्यों नहीं बना सकता, बोलिए तो ?
यदि हजारों लोग किसी निरंजन सिंह को निरोंजोन भट्टाचार्ज्या बताने लगें तो किसी के, और तो और निरंजन बाबू की अर्द्धांगिनी तक के आपत्ति करने से समाज में उस व्यक्ति की निरंजन भट्टाचार्ज्या के रूप में प्रतिष्ठा रुक सकेगी क्या विशेष रूप से तब जबकि उन हजारों लोगों में से कुछ निरंजन बाबू के निकट सम्बन्धी भी हों ? मेरे विषय में तो अनेकानेक लोगों का मानना है कि मैं उस व्यक्ति का-सा ही दिखता हूँ जिसका नाम मैं ‘कौन?’ पूछे जाने पर उचारता हूँ। किन्तु यदि मैं उससे सर्वथा भिन्न भी दिखता होता तो भी उससे कोई अन्तर न पड़ता। इसका दृष्टान्त मिलता है पिछली सदी में विलायत में हुए विख्यात टिचबोर्न केस से। कहीं आप यह न समझ बैठें कि मैं कोई बैरिस्टर-टैरिस्टर हूँ।
टिचबोर्न केस का नाम तो मैंने पहली बार तब सुना जब वर्षों तक चलते रहने के बाद मैंने अपने समर्थकों के आग्रह के समक्ष शीश नवाकर अपनी अस्मिता की वापसी के लिए उस भद्र महिला पर मुकदमा पर मुकदमा ठोंक दिया जिसे मैं अपनी धर्मपत्नी मानता हूँ। केस फाइल करने के बाद मेरे वकील बैरिस्टर चटर्जी बोले, आपका यह मुकदमा भारत का टिचबोर्न कहलाएगा और उतना ही ख्यात भी होगा। मेरे जिज्ञासा करने पर उन्होंने बताया कि एक धनाढ्य सामन्त लार्ड टिचबोर्न का एकमात्र पुत्र रॉजर 1854 में रिओ डि जोनारिया से जमाइका जाते हुए जहाज डूबने पर जलसमाधि पा गया था। तो 1866 में लार्ड टिचबोर्न की मृत्यु के बाद उनका भतीजा आर्थर उनका उत्तराधिकारी बना। तभी लेडी टिचबोर्न को आस्ट्रेलिया से किसी टॉमस कास्ट्रो का पत्र मिला कि मैं तुम्हारा वही अयोग्य पुत्र हूँ जो घर छोड़कर दक्षिण अमेरिका चला गया था। मेरा जहाज डूब गया था किन्तु मछली पकड़ने वाले एक अन्य जहाज के नाविकों ने मुझे बचा लिया और अपने साथ न्यू साउथ वेल्स ले आए। तब से मैं यहीं हूँ। हाल ही में पिताजी की मृत्यु का दुखद समाचार सुनने को मिला। मैं तुमसे मिलने आना चाहता हूँ किन्तु मैं यहाँ इतनी गरीबी में जी रहा हूँ कि इंग्लैंड का टिकट खरीदना मेरे सामर्थ्य से बाहर है।
लेडी टिचबोर्न ने कास्ट्रो से पत्र-व्यवहार किया। आश्वस्त हुई कि वह रॉजर ही है। पैसा भेजकर उसे बुला लिया।
यद्यपि कास्ट्रो थुल-थुला जबकि रॉजर दुबला-पतला, कास्ट्रो फूहड़ था जबकि रॉजर परिष्कृत और कास्ट्रो सामन्ती आचार-व्यवहार से अनभिज्ञ था जबकि रॉजर को वे संस्कार में मिले थे न केवल लेडी टिचबोर्न ने वरन् समस्त कृषकों ने कास्ट्रो को रॉजर मान लिया। आर्थर समेत अन्य सम्बन्धियों के यह पता कर लेने से भी कोई अन्तर न पड़ा कि कास्ट्रो आस्ट्रेलिया में पहले आर्थर ऑर्टन के नाम से भी जाना जाता रहा है। और उसे रॉजर की भूमिका में उतारने की सूझ सिडनी के एक ठग मिस्टर बोगले की है। कास्ट्रो के इंग्लैंड पहुँचने के दो वर्ष बाद 1869 में लेडी टिचबोर्न का देहांत हो गया और आर्थर ने कास्ट्रो के टिचबोर्न होने का दावा प्रस्तुत किया। बैरिस्टर चटर्जी इस केस में हुए अदालती दाँव-पेंचों पर अवश्य प्रकाश डालते किन्तु मेरा मन कथा-कहानी में अधिक लगता नहीं। अस्तु टोक कर कहा कि कास्ट्रो केस जीता कि हारा ? वह बोले कि हारा और इस पराजय के बाद भी प्रजाजन उसे और वह स्वयं को रॉजर टिचबोर्न ही बताता रहा इसलिए उस पर फौजदारी केस बनाया गया और उसे 14 वर्ष का कारावास का दण्ड दिया गया।
मैंने हँसकर पूछा, ‘तो क्या यह मुकदमा मुझे 14 वर्ष के कारावास पर भिजवाने के लिए दायर करवाया है आप लोगों ने।’ अच्छा नहीं लगा यह परिहास मेरे समर्थकों और वकीलों को। चटर्जी मोशाय बोले, ‘आपकी ओर से तो दीवानी मुकदमा दायर किया है। दंड का प्रश्न तो तब उठेगा जब यह मुकदमा न जीत पाने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ चुकने के बाद भी आप अपने को उन भद्र महिला का पति बताते रहें जिन पर आपने यह मुकदमा दायर किया है। मैंने पुनः हँसते हुए जिज्ञासा की कि उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के आ जाने की कितनी आशंका है। वह बोले, ‘उसे न आने देने के लिए यथासंभव, यथासामर्थ्य प्रयत्न करूँगा मैं किन्तु स्पष्ट कर दूँ कि जहाँ तक मुझे ज्ञात है अस्मिता सम्बन्धी किसी मुकदमे में आज तक कोई दावेदार विजयी हुआ नहीं है क्योंकि अस्मिता सिद्ध लगी है किन्तु आप अपने को जो व्यक्ति बता रहे हैं दुर्भाग्य से उसकी अंगुलियाँ के निशान लिये जाने का कोई अवसर कभी आया न था।
मैंने फिर हँसकर कहा कि उसके अंगुलियों के निशान का रिकार्ड न होना आप वकीलों के लिए तो सौभाग्य का विषय है। सदा गंभीर रहने वाले चटर्जी मोशाय अब थोड़ा-सा मुस्कराए। बोले, वकीलों के लिए तो हर स्थिति सौभाग्यपूर्ण होती है। उस व्यक्ति के अंगुलियों के निशान होते पुलिस या प्रशासन के पास तो भी वाद-विवाद की पूरी संभावना रहती। यदि आपकी अंगुलियों के निशान न मिलते तो मैं या तो सिद्ध करता कि ये निशान उस व्यक्ति के हैं ही नहीं। या यह कि विशेषज्ञ ने गलत रिपोर्ट दी है। और मिल जाते तो उन भद्र महिला के वकील भी ठीक यही प्रयास करते।
इस मुकदमे में तो अस्मिता सिद्ध करने का कोई उपाय है ही नहीं जो सबको मान्य हो सके। आप यह न भूलें कि आप अपने को जो व्यक्ति बता रहे हैं उसके दाह-संस्कार का सरकारी प्रमाण-पत्र उपलब्ध है। मेरा एक समर्थक बोला कि उस प्रमाण-पत्र के झूठे होने का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है बैरिस्टर साहब कि जिसका दाह संस्कार कर दिया गया था वह हमारे सामने साक्षात उपस्थित है। चटर्जी मोशाय बोले कि यह उसका-सा दीखने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी तो हो सकता है। जुड़वा तो बिल्कुल एक-से दिखते हैं। क्या यह असम्भव है कि एक जुड़वाँ का दाह-संस्कार कर दिया जाए और दूसरा उसकी संपत्ति का दावेदार बनने के लिए उसकी अस्मिता ओढ़ ले। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को कोई और समझकर पुकार लेते हैं और बाद में पाते हैं कि वह तो कोई हमारे परिचित का हमशक्ल कोई अजनबी है। अस्मिता की समरूपता सिद्ध करने के लिए एक ही कसौटी बचती है कि दोनों व्यक्तियों का तन ही नहीं, मन-मस्तिष्क भी एक-सा हो। आप जो व्यक्ति होने का दावा कर रहे हो उसकी तमाम स्मृतियाँ आपके भीतर उपस्थित हों क्योंकि आप जिसे आप कहते हैं वह आपकी अब तक की राम कहानी की स्मृतियों का समग्र प्रभावभर होता है।
मैंने कहा, ‘मेरे गुरु कहा करते थे कि इंसान यादों की औलाद होता है।’ चटर्जी मोशाय बोले, ‘वही तो। किन्तु यादों का भी ऐसा है कि बनती-मिटती रहती हैं। और हाँ, यादें इस अर्थ में उधार भी ली जा सकती हैं कि आप जो व्यक्ति होने का दावा कर रहे हों उसके जीवन की घटनाओं के बारे में दूसरों से पता कर लें। इसलिए अस्मिता का प्रश्न बड़ा जटिल है।’ तो आप बूझ ही गए होंगे पाठकगण कि क्यों मैंने कहा कि आप नितान्त सौभाग्यशाली हैं कि लोगों को आपके आप होने के विषय में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आपके ‘के?’ के उत्तर में ‘आमि’ उचारते ही पत्नी बन्द कपाट खोल देती है। इस सामान्य-से अधिकार के लिए मुझे अदालत की शरण में जाना पड़ रहा है। मैं इसी विचित्र व्यापार की कथा लिखने बैठा हूँ।
मैं मिथ्या बोल गया। लिखने नहीं बैठा हूँ, लिखवा रहा हूँ। लिखना-पढ़ना वो सब आता नहीं है मुझे। मैं और जिन भद्र महिला पर मैंने मुकदमा दायर किया है (अर्थात् मेरी धर्मपत्नी बिभा देबी) बस इसी विषय में सहमत हैं कि मैं निरक्षर भट्टाचार्य हूँ। यह कथा लिखनेवाने की विशेष इच्छा नहीं थी मेरी किन्तु बोऊदी का सिफारिशी पत्र लेकर तरुण पत्रकार निरंजन भट्टाचार्ज्या आ गए हैं और कह रहे हैं कि आपके बारे में आपसे अनुमति लिए और परामर्श किए बगैर अनगिनत छोटी-मोटी पुस्तकें होती रही हैं पिछले कुछ वर्षों से। मेरी इच्छा है कि आपकी सहायता से इस बार मैं कोई प्रामाणिक और साहित्यिक कृति तैयार करूँ।
अपनी साहित्यिक क्षमता के प्रमाण स्वरूप निरंजन बाबू ‘ढाका प्रकाश’, ‘अमृत बाजार पत्रिका’ आदि में छपे अपने लेखों की कतरनों की फाइल लेकर आए हैं। मैंने इनसे कहा है कि यह फाइल तो आप बिभा देबी को ही दिखाएँ। साहित्यानुरागी वही है। और हाँ, आप जो भी लिखें, मुझसे ही नहीं, उनसे भी परामर्श करके लिखें। मेरे गुरु कह करते थे कि इस संसार का हर सच तब तक झूठ होता है पुत्त्र जब तक कि उसे अदालत में जाकर सच न साबित कर दिया जावे। और तब भी वह उसके लिए सच नहीं होता जो मुकदमे में हार जाता है। तो निरंजन बाबू मेरे झूठ के साथ बिभा देबी का झूठ भी सुनते रहिएगा।
बहुधा इतना पर्याप्त होता है पट खोल दिए जाने के लिए। किन्तु यदि भीतर वाला स्वभाव से शंकालु हो अथवा इधर जाली परिचय देकर द्वार खुलवा लेने और लूटकर चले जाने की कुछ घटनाएँ चर्चा में रही हों तो सम्भव है कि पट बन्द ही रहें। उत्तर चाहे तो भीतरवाले के अविश्वास को निर्मूल सिद्ध करने का यत्न करते रह सकता है। किन्तु वह अविश्वास और आशंका निर्मूल नहीं। इस असार संसार में पग-पग पर धोखे हैं। बोलबाला है ठग विद्या का। कोई लुटेरा-हत्यारा कहीं से यह पूछकर आ गया हो सकता है कि गृहस्वामी के जमाई बाबू के भांजे का नाम निरंजन भट्टाचार्या है। पछताने से अच्छा है पछतावे की नौबत ही न आने देना। यदि आगंतुक वास्तव में जमाई बाबू का भांजा ही सिद्ध हो तो उससे और जमाई बाबू से क्षमा-याचना की जा सकती है बाद में। बुद्धिमत्ता इसी मैं है कि जो ‘के’ के उत्तर में ‘आमि’ कह रहा हो उसका ‘आमि’ को परिभाषित और परिसीमित कर देना अपर्याप्त माना जाए। उससे यह प्रमाणित करने को कहा जाए कि उस परिभाषा और परिसीमन से जो व्यक्ति निरूपित होता है वह सचमुच उसकी काया में बसता है। सभी सरकारी व्यापारों में पहचानपत्रों, हलफनामों हस्ताक्षरों, अंगूठा-निशानों को यूँ ही तो अनिवार्य नहीं बना दिया गया है ना।
तो पाठकगण आप उस बन्द द्वार की साँकल की ओर हाथ बढ़ाते हुए एक क्षण ठिठकर सोच लिया करें कि चुनौती मिलने की स्थिति में आप अपने ‘आमि’ को प्रमाणित कर सकने की किसी युक्ति से लैस हैं कि नहीं ? यथा मैं वही निरंजन हूँ जिसने मामा के यहाँ आपका बनाया हुआ कटहल का अचार इतने स्वाद से खाया था कि मामी-माँ अगली बार मायके से लौटीं तो एक अमृतबान मेरे लिए भी भरवा लाईं उसका। और यदि इस पर भी द्वार न खुले तो यह कि मैं तो आपको आपके जमाई बाबू का एक पत्र देने आया था। चलिए द्वार के नीचे से सरका देता हूँ, नमस्कार। इधर पत्र खोलकर हस्ताक्षर देखे जमाई बाबू के कि उधर द्वार खोलकर आपको पुकार लिया जाएगा क्षमा-याचनाओं की झड़ी लगाते हुए। यों यदि द्वार के उस पार का व्यक्ति छाछ को भी फूँक-फूँककर पीने के लिए बाध्य कर दिया जा चुका हो तो वह यह सोचकर द्वार न खोलना ही उचित समझा जाता है कि कटहल के अचार वाला प्रसंग किसी और को भी पता हो सकता है तथा जाली हस्ताक्षरों के केस तो प्रायः होते ही रहते हैं। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि हर व्यक्ति को तब तक जाली ही समझा जाए जब तक कि वह अपना असली होना प्रमाणित न कर दे और इसके साथ ही इस बात को कदापि न भुलाया जाए कि प्रमाण भी जाली, भ्रामक और झूठे हो सकते हैं। मेरे गुरु बाबा धर्मदास कहा करते थे कि महाठगिनी माया का जाल है यह संसार और इसमें सब कुछ जाली और झूठा है।
विश्वास मानिए पाठकगण कि जब-जब आप किसी शंकालु के घर के बन्द द्वार की साँकल की ओर हाथ बढ़ा रहे होंगे तब-तब मेरी सहानुभूति आप पर पंखा झल रही होगी। मैं तो आपसे कहीं अधिक दयनीय स्थिति में हूँ। आप जब अपने घर का द्वार खटखटाते हैं तब भीतर से पत्नी द्वारा पूछे गए ‘के ?’ के उत्तर में आपका ‘आमि’ कह देना न केवल पर्याप्त रहता होगा वरन् आप भीतर चरण रखते हुए यह टिप्पणी करने को स्वतंत्र मानते होंगे अपने को कि क्यों व्यर्थ के प्रश्न करती हो, इस वेला और कौन आता है यहाँ ? किन्तु यदि कहीं मेरे और उस स्त्री के मध्य कोई बन्द द्वार हो जिससे मैं सात फेरे लेकर बँधा हुआ हूँ तो साँकल की ओर बढ़ते मेरे हाथ यह सोचकर ठिठक जाएँगे कि उसकी ‘के?’ के उत्तर में अपने ‘आमि’ को किस प्रकार परिभाषित करना उचित होगा मेरे लिए ? यदि यह कहूँ कि तुम्हारा स्वामी हूँ तो वह क्यों खोलेगी भला जबकि सार्वजनिक रूप से घोषित कर चुकी है कि मेरे पति का देहान्त हो चुका है ? द्वार खोलकर एक ठो भूत को कौन स्त्री अपना भविष्य बनाना चाहेगी, बोलिए तो। और यदि मैं यह कहूँ कि मैं वह ठग हूँ जो अपने को तुम्हारा पति बताता घूम रहा है तो वह पुलिस को ही बुलाएगी ना। शासकीय निषेध है मेरे उस भद्र महिला की बाड़ी के आस-पास जाने पर।
आमि-आमि का सतत जाप करते पाठकगण सावधान। आप तभी तक आप हैं जब तक दूसरे आपको आप मान रहे हैं। और सकल व्यापार में चिन्ता करते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे किन्तु इस विषय में कभी चिन्तित नहीं होते कि लोग आप को आप नहीं कहेंगे तब क्या गति होगी आपकी ? कल्पना कीजिए मैं यह गाथा लिख नहीं रहा हूँ, सुना रहा हूँ आपको वैसे ही एक विराट मैदान में जिसमें जयदेवपुर की राजबाड़ी का पोलो ग्राउण्ड था। मैं आपमें से एक की ओर तर्जनी उठाकर जिज्ञासा करता हूँ, ‘आपनि के ?’ और वह एक उत्तर देता है, ‘आमि निरोंजोन भट्टाचार्ज्या।’ और तभी क्या होता है कि आपमें से कुछ हँसकर और कुछ क्रुद्ध होकर सूचित करते हैं मुझे कि यह निरंजन भट्टाचार्ज्या नहीं हैं। मैं उस व्यक्ति को पागल अथवा ठग मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाऊँगा क्या ? पागल तो अपने को कुछ भी मान लेते हैं। जयदेवपुर के पगले दीपेन बाबू तो अपने को क्वीन विक्टोरिया कहते डोलते थे। ठगों का तो काम ही किसी अन्य की अस्मिता ओढ़ लेना है। अब कल्पना कीजिए कि वह श्रोता-विशेष न ठग था, न पागल। वह तो वास्तव में जन्मजात निरंजन भट्टाचार्ज्या ही था किन्तु अन्य लोगों ने किसी कारणवश उसकी अस्मिता निरस्त कर डालने का एक विराट षड्यन्त्र रच रखा था। ऐसे में वह मेरे लिए या किसी के लिए भी निरंजन भट्टाचार्ज्या रह सकता था भला ? उस एक अकेले की बात उन अन्य हजारों की बात के आगे ठहर सकती है भला ? अकाट्य होता है संख्या का तर्क। तो निरंजन भट्टाचार्ज्या आप सभी पाठकगण प्रभु का धन्यवाद करते रहें कि आपको निरोंजोन भट्टाचार्ज्या आमि ही मान रहे हैं सब जन। कहीं यह नहीं कहा जा रहा है कि आप बंगभूमि के छेले न होकर पंजाब दे पुत्तर निरंजन सिंह हैं। और जाल अर्थात् जाली निरोंजोन भट्टाचार्ज्या बने घूम रहे हैं।
कृपया यह न समझें कि मैं अपनी पत्नी पर यह आक्षेप लगाना चाहता हूँ कि उसने मेरी अस्मिता की व्यापक अस्वीकृति के लिए कोई विराट षड्यन्त्र रचा है। वस्तुस्थिति तो यह है कि वह ऐसा समझती है या उसे समझा दिया गया है कि कुछ स्वार्थी लोगों ने एक ठो अपात्र पर मेरे दिवंगत पति की अस्मिता आरोपित कर देने का विराट षड्यन्त्र रचा है। उस बेचारी के मन में ऐसी आशंका उठना स्वाभाविक है। और पाठकगण जब आप का आप होना दूसरों के आप को आप मानने पर निर्भर है अंततः तब संख्या का तर्क जैसे असली निरंजन भट्टाचार्ज्या को जाली सिद्ध कर सकता है तब जाली निरंजन भट्टाचार्ज्या को असली क्यों नहीं बना सकता, बोलिए तो ?
यदि हजारों लोग किसी निरंजन सिंह को निरोंजोन भट्टाचार्ज्या बताने लगें तो किसी के, और तो और निरंजन बाबू की अर्द्धांगिनी तक के आपत्ति करने से समाज में उस व्यक्ति की निरंजन भट्टाचार्ज्या के रूप में प्रतिष्ठा रुक सकेगी क्या विशेष रूप से तब जबकि उन हजारों लोगों में से कुछ निरंजन बाबू के निकट सम्बन्धी भी हों ? मेरे विषय में तो अनेकानेक लोगों का मानना है कि मैं उस व्यक्ति का-सा ही दिखता हूँ जिसका नाम मैं ‘कौन?’ पूछे जाने पर उचारता हूँ। किन्तु यदि मैं उससे सर्वथा भिन्न भी दिखता होता तो भी उससे कोई अन्तर न पड़ता। इसका दृष्टान्त मिलता है पिछली सदी में विलायत में हुए विख्यात टिचबोर्न केस से। कहीं आप यह न समझ बैठें कि मैं कोई बैरिस्टर-टैरिस्टर हूँ।
टिचबोर्न केस का नाम तो मैंने पहली बार तब सुना जब वर्षों तक चलते रहने के बाद मैंने अपने समर्थकों के आग्रह के समक्ष शीश नवाकर अपनी अस्मिता की वापसी के लिए उस भद्र महिला पर मुकदमा पर मुकदमा ठोंक दिया जिसे मैं अपनी धर्मपत्नी मानता हूँ। केस फाइल करने के बाद मेरे वकील बैरिस्टर चटर्जी बोले, आपका यह मुकदमा भारत का टिचबोर्न कहलाएगा और उतना ही ख्यात भी होगा। मेरे जिज्ञासा करने पर उन्होंने बताया कि एक धनाढ्य सामन्त लार्ड टिचबोर्न का एकमात्र पुत्र रॉजर 1854 में रिओ डि जोनारिया से जमाइका जाते हुए जहाज डूबने पर जलसमाधि पा गया था। तो 1866 में लार्ड टिचबोर्न की मृत्यु के बाद उनका भतीजा आर्थर उनका उत्तराधिकारी बना। तभी लेडी टिचबोर्न को आस्ट्रेलिया से किसी टॉमस कास्ट्रो का पत्र मिला कि मैं तुम्हारा वही अयोग्य पुत्र हूँ जो घर छोड़कर दक्षिण अमेरिका चला गया था। मेरा जहाज डूब गया था किन्तु मछली पकड़ने वाले एक अन्य जहाज के नाविकों ने मुझे बचा लिया और अपने साथ न्यू साउथ वेल्स ले आए। तब से मैं यहीं हूँ। हाल ही में पिताजी की मृत्यु का दुखद समाचार सुनने को मिला। मैं तुमसे मिलने आना चाहता हूँ किन्तु मैं यहाँ इतनी गरीबी में जी रहा हूँ कि इंग्लैंड का टिकट खरीदना मेरे सामर्थ्य से बाहर है।
लेडी टिचबोर्न ने कास्ट्रो से पत्र-व्यवहार किया। आश्वस्त हुई कि वह रॉजर ही है। पैसा भेजकर उसे बुला लिया।
यद्यपि कास्ट्रो थुल-थुला जबकि रॉजर दुबला-पतला, कास्ट्रो फूहड़ था जबकि रॉजर परिष्कृत और कास्ट्रो सामन्ती आचार-व्यवहार से अनभिज्ञ था जबकि रॉजर को वे संस्कार में मिले थे न केवल लेडी टिचबोर्न ने वरन् समस्त कृषकों ने कास्ट्रो को रॉजर मान लिया। आर्थर समेत अन्य सम्बन्धियों के यह पता कर लेने से भी कोई अन्तर न पड़ा कि कास्ट्रो आस्ट्रेलिया में पहले आर्थर ऑर्टन के नाम से भी जाना जाता रहा है। और उसे रॉजर की भूमिका में उतारने की सूझ सिडनी के एक ठग मिस्टर बोगले की है। कास्ट्रो के इंग्लैंड पहुँचने के दो वर्ष बाद 1869 में लेडी टिचबोर्न का देहांत हो गया और आर्थर ने कास्ट्रो के टिचबोर्न होने का दावा प्रस्तुत किया। बैरिस्टर चटर्जी इस केस में हुए अदालती दाँव-पेंचों पर अवश्य प्रकाश डालते किन्तु मेरा मन कथा-कहानी में अधिक लगता नहीं। अस्तु टोक कर कहा कि कास्ट्रो केस जीता कि हारा ? वह बोले कि हारा और इस पराजय के बाद भी प्रजाजन उसे और वह स्वयं को रॉजर टिचबोर्न ही बताता रहा इसलिए उस पर फौजदारी केस बनाया गया और उसे 14 वर्ष का कारावास का दण्ड दिया गया।
मैंने हँसकर पूछा, ‘तो क्या यह मुकदमा मुझे 14 वर्ष के कारावास पर भिजवाने के लिए दायर करवाया है आप लोगों ने।’ अच्छा नहीं लगा यह परिहास मेरे समर्थकों और वकीलों को। चटर्जी मोशाय बोले, ‘आपकी ओर से तो दीवानी मुकदमा दायर किया है। दंड का प्रश्न तो तब उठेगा जब यह मुकदमा न जीत पाने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ चुकने के बाद भी आप अपने को उन भद्र महिला का पति बताते रहें जिन पर आपने यह मुकदमा दायर किया है। मैंने पुनः हँसते हुए जिज्ञासा की कि उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के आ जाने की कितनी आशंका है। वह बोले, ‘उसे न आने देने के लिए यथासंभव, यथासामर्थ्य प्रयत्न करूँगा मैं किन्तु स्पष्ट कर दूँ कि जहाँ तक मुझे ज्ञात है अस्मिता सम्बन्धी किसी मुकदमे में आज तक कोई दावेदार विजयी हुआ नहीं है क्योंकि अस्मिता सिद्ध लगी है किन्तु आप अपने को जो व्यक्ति बता रहे हैं दुर्भाग्य से उसकी अंगुलियाँ के निशान लिये जाने का कोई अवसर कभी आया न था।
मैंने फिर हँसकर कहा कि उसके अंगुलियों के निशान का रिकार्ड न होना आप वकीलों के लिए तो सौभाग्य का विषय है। सदा गंभीर रहने वाले चटर्जी मोशाय अब थोड़ा-सा मुस्कराए। बोले, वकीलों के लिए तो हर स्थिति सौभाग्यपूर्ण होती है। उस व्यक्ति के अंगुलियों के निशान होते पुलिस या प्रशासन के पास तो भी वाद-विवाद की पूरी संभावना रहती। यदि आपकी अंगुलियों के निशान न मिलते तो मैं या तो सिद्ध करता कि ये निशान उस व्यक्ति के हैं ही नहीं। या यह कि विशेषज्ञ ने गलत रिपोर्ट दी है। और मिल जाते तो उन भद्र महिला के वकील भी ठीक यही प्रयास करते।
इस मुकदमे में तो अस्मिता सिद्ध करने का कोई उपाय है ही नहीं जो सबको मान्य हो सके। आप यह न भूलें कि आप अपने को जो व्यक्ति बता रहे हैं उसके दाह-संस्कार का सरकारी प्रमाण-पत्र उपलब्ध है। मेरा एक समर्थक बोला कि उस प्रमाण-पत्र के झूठे होने का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है बैरिस्टर साहब कि जिसका दाह संस्कार कर दिया गया था वह हमारे सामने साक्षात उपस्थित है। चटर्जी मोशाय बोले कि यह उसका-सा दीखने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी तो हो सकता है। जुड़वा तो बिल्कुल एक-से दिखते हैं। क्या यह असम्भव है कि एक जुड़वाँ का दाह-संस्कार कर दिया जाए और दूसरा उसकी संपत्ति का दावेदार बनने के लिए उसकी अस्मिता ओढ़ ले। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को कोई और समझकर पुकार लेते हैं और बाद में पाते हैं कि वह तो कोई हमारे परिचित का हमशक्ल कोई अजनबी है। अस्मिता की समरूपता सिद्ध करने के लिए एक ही कसौटी बचती है कि दोनों व्यक्तियों का तन ही नहीं, मन-मस्तिष्क भी एक-सा हो। आप जो व्यक्ति होने का दावा कर रहे हो उसकी तमाम स्मृतियाँ आपके भीतर उपस्थित हों क्योंकि आप जिसे आप कहते हैं वह आपकी अब तक की राम कहानी की स्मृतियों का समग्र प्रभावभर होता है।
मैंने कहा, ‘मेरे गुरु कहा करते थे कि इंसान यादों की औलाद होता है।’ चटर्जी मोशाय बोले, ‘वही तो। किन्तु यादों का भी ऐसा है कि बनती-मिटती रहती हैं। और हाँ, यादें इस अर्थ में उधार भी ली जा सकती हैं कि आप जो व्यक्ति होने का दावा कर रहे हों उसके जीवन की घटनाओं के बारे में दूसरों से पता कर लें। इसलिए अस्मिता का प्रश्न बड़ा जटिल है।’ तो आप बूझ ही गए होंगे पाठकगण कि क्यों मैंने कहा कि आप नितान्त सौभाग्यशाली हैं कि लोगों को आपके आप होने के विषय में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आपके ‘के?’ के उत्तर में ‘आमि’ उचारते ही पत्नी बन्द कपाट खोल देती है। इस सामान्य-से अधिकार के लिए मुझे अदालत की शरण में जाना पड़ रहा है। मैं इसी विचित्र व्यापार की कथा लिखने बैठा हूँ।
मैं मिथ्या बोल गया। लिखने नहीं बैठा हूँ, लिखवा रहा हूँ। लिखना-पढ़ना वो सब आता नहीं है मुझे। मैं और जिन भद्र महिला पर मैंने मुकदमा दायर किया है (अर्थात् मेरी धर्मपत्नी बिभा देबी) बस इसी विषय में सहमत हैं कि मैं निरक्षर भट्टाचार्य हूँ। यह कथा लिखनेवाने की विशेष इच्छा नहीं थी मेरी किन्तु बोऊदी का सिफारिशी पत्र लेकर तरुण पत्रकार निरंजन भट्टाचार्ज्या आ गए हैं और कह रहे हैं कि आपके बारे में आपसे अनुमति लिए और परामर्श किए बगैर अनगिनत छोटी-मोटी पुस्तकें होती रही हैं पिछले कुछ वर्षों से। मेरी इच्छा है कि आपकी सहायता से इस बार मैं कोई प्रामाणिक और साहित्यिक कृति तैयार करूँ।
अपनी साहित्यिक क्षमता के प्रमाण स्वरूप निरंजन बाबू ‘ढाका प्रकाश’, ‘अमृत बाजार पत्रिका’ आदि में छपे अपने लेखों की कतरनों की फाइल लेकर आए हैं। मैंने इनसे कहा है कि यह फाइल तो आप बिभा देबी को ही दिखाएँ। साहित्यानुरागी वही है। और हाँ, आप जो भी लिखें, मुझसे ही नहीं, उनसे भी परामर्श करके लिखें। मेरे गुरु कह करते थे कि इस संसार का हर सच तब तक झूठ होता है पुत्त्र जब तक कि उसे अदालत में जाकर सच न साबित कर दिया जावे। और तब भी वह उसके लिए सच नहीं होता जो मुकदमे में हार जाता है। तो निरंजन बाबू मेरे झूठ के साथ बिभा देबी का झूठ भी सुनते रहिएगा।
आमि कोथाय एलाम ?
धर्मदास कुछ नहीं था। कुछ न होने का बोध भी नहीं। मानो अस्तित्वहीनता के अचल अन्धकारमय जल में डूबा हुआ था मैं। फिर अनुभूति हुई कि कोई सशक्त हाथ मझे ऊपर खींच ले जाने का यत्न कर रहे हैं। प्रकाश-सा दिखाई पड़ा। कुछ समय लगा मेरी आँखों को प्रकाश की अभ्यस्त होने में। हुईं तो पाया कि मेरे ऊपर टीन का छप्पर है। मैं अशक्त लेटा हुआ हूँ एक ढीली-सी खटिया पर, दो-दो कम्बल ओढ़े। अच्छा तो ज्वर-जन्य गहन निद्रा से जागा हूँ मैं। कदाचित् इसीलिए धुएँ की गन्ध से भरा यह स्थान और मेरी और बड़े कुतूहल से देखते ये जटाजूट एवं भस्मलेपधारी चार नागा साधु अपरिचित-से लग रहे हैं मुझे। सूखे ओठों पर जीभ फेरने के बाद जिज्ञासा की मैंने कि आमि कोथाय एलाम ?
मैं कहाँ आ गया हूँ। सुनकर उन साधुओं के चेहरे चमक उठे सुख-सन्तोष से। मैं दुहराता गया अपना प्रश्न। तब एक साधु ने ओठों पर अँगुली रखकर मुझे चुप रहने का निर्देश दिया। साधुओं ने आपस में बातें कीं अपनी भाषा में और उसी में मुझसे कुछ पूछा भी। ना, यह कथन तो भ्रामक है भयंकर रूप से। मुझे तब यह बोध न था कि मैं एक भाषा में बोला था और वे दूसरी बोल रहे हैं और ये भाषाएँ क्रमशः बांग्ला और हिन्दी कहलाती हैं। मेरी संज्ञा लौट आई थी किन्तु भेद-बुद्धि नहीं। सब कुछ एक समान था मेरे लिए। आकाश और पाताल, जड़ और चेतन, स्त्री और पुरुष, श्वेत और श्याम, गृहस्थ और साधु, किसी में भी कोई अन्तर नहीं कर पा रहा था मैं तब।
संज्ञा लौट आने के अनेक मास बाद तक भी यही स्थिति रही मेरी। मुझे कोई अन्तर न लगा उन साधुओं और अपने में, उनकी भाषा में और अपनी भाषा में। भाषा की कोई आवश्यकता न थी मेरे लिए। कुछ था ही नहीं बताने-पूछने को। ‘आमि कोथाय एलाम ?’ का वह प्रश्न पूछना भी छोड़ दिया मैंने। नवजात शिशु के स्तर पर ही पहुँच पाई थी तब तक मेरी चेतना। ना, नवजात शिशु भी उतना गूँगा-बहरा और अपने आस-पास को स्मृति में अंकित कर सकने में उतना असमर्थ नहीं होता जितना कि मैं था तब। मात्र इसी अर्थ में शिशु सिद्ध न हुआ मैं कि कुछ ही दिनों में उठने-बैठने, चलने-फिरने लगा। शिशु को तो प्रायः वर्ष-डेढ़ वर्ष लग जाते हैं।
‘कुछ ही दिनों’ की यह कथा भी सुनी मात्र सुनी-सुनाई है। काल के मुँह में पहुँचने की प्रक्रिया में अपना कालबोध भी गँवा बैठा था मैं। तो समय की सुइयाँ चलती रहीं, मैं भी चलता रहा साधुओं के साथ यन्त्रवत्, दिवस-मास बीतते गये, बदलता गया परिवेश। किन्तु मुझे इसका कोई ज्ञान न हुआ। वयोवृद्ध साधु मुझे बच्चा कहकर सम्बोधित करते रहे। पालते रहे मुझ असहाय को किसी सदय माँ की भाँति। वही मुझे औषधि देते, खाना खिलाते, शौच और स्नान कराते। वे जैसा कहते, मैं करता जाता। जैसे मेरी कोई अपनी इच्छा ही शेष न रह गई हो। सुनने में आपको विचित्र लगेगा किन्तु यह सत्य है कि बनारस पहुँचने तक मुझे यह भी चेतना न थी कि मैं मनुष्य हूँ कि पशु कि पाषाण कि पक्षी ?
मैं अपना ही नहीं, सभी प्राणियों, पदार्थों का नाम भूल चुका था। बनारस हम कब पहुँच गए, कैसे पहुँच गए इसका भी कोई भान न हो सका मुझे। बनारस पहुँचकर मन्द-मन्थर गति से लौटी चेतना। समझ पाया अन्ततः कि राँड़-साँड सीढ़ी संन्यासी भिन्न है एक-दूसरे से।
लेकिन इतनी चेतना नहीं लौटी कि समझ सकूँ कि मुझमें और मेरे साथियों में कोई विशेष अन्तर है। काशी में हमने एक मठ में डेरा किया। नगर में प्रवासी बंगालियों की काफी बड़ी आबादी होने के कारण मुझे बांग्ला बहुत सुनने को मिलने लगी। मुझे वह अतिपरिचित भाषा लगी और मैंने यह पाया कि स्वयं भी उसे बोल पाता हूँ, किन्तु मेरे मन में यह बात बिल्कुल नहीं उठी कि मैं बंगाली हूँ और बांग्ला मेरी मातृभाषा है। दो बंगाली साधुओं ने मुझसे बात की और जानना चाहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ। मैं जानता होता तब न बताता। मेरे तन भले ही साधुओं की जड़ी-बूटियों के चमत्कार से स्वस्थ होता चला गया हो, मन अब भी अस्वस्थ ही चल रहा था कदाचित्। ऐसा मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं अपनी स्मृति खो बैठा था बल्कि इसलिए कि अपनी खोई स्मृति खोजने की कोई उत्कण्ठा न थी मेरे मन में।
मैं घाट पर अपने साथ के बाबाजी और अन्य साधु सन्तों के प्रवचन सुनता रहता किन्तु वे भी मेरे शिथिल मन में कोई स्फूर्ति जगा न पाते। मैं पथराई आँखों से इधर-उधर देखता रहता और कभी-कभी पाता कि कुछ जोड़ा अन्य आँखों भी मुझे देख रही हैं बहुत विस्मय से। मानो प्रयास कर रही हों मुझे पहचानने का। बहुधा मुझे भी अपने को इसी प्रकार घूरने वाला व्यक्ति परिचित-सा प्रतीत होता। एक दिन हम लोग घाट पर बैठे हुए थे कि किसी परिचित-से लगते अपरिचित ने दूर से मुझे बड़े कुतूहल से देखा। फिर वह मेरे पास आया और उसकी आँखों में विस्मय का भाव गहराता गया। उसने मुझसे कहा बांग्ला में आप और इस भेस में ? मैं कुछ समझा नहीं। कह दिया कि साधु तो साधु के भेस में ही होगा। बोला, ‘जान सकता हूँ कि आप साधु बनने से पहले कौन थे, कहाँ थे ?’ मैं साधु बनने का रहस्य समझ नहीं पाया। पूछा, ‘आप क्या कहना चाहते हैं ?’ उसने प्रश्न फिर दुहराया लेकिन मेरा उत्तर तो वही हो सकता था जो पहले दे चुका था। तो वह जाकर हमारी टोली के मुखिया से बात करने लगा। उसी रात हमने बनारस से प्रस्थान कर दिया। विन्ध्याचल पहुँचकर धूनी रमाई। वहीं विन्ध्यवासिनी देवी की अनुकम्पा से मेरी चेतना लगभग भाषाहीन बच्चे से कुछ ऊपर उठी।
मैं पहली बार समझ पाया कि जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ उनसे भिन्न हूँ। वे उदासीन पन्थ के साधु हैं जबकि मैं नहीं हूँ। वे पंजाबी हैं और मैं कदाचित् बंगाली हूँ क्योंकि बांग्ला मुझे अच्छी तरह समझ में आती है जबकि इन लोगों की पंजाबी नहीं। मैं इनकी तरह हिन्दी बोल लेता हूँ लेकिन मेरी हिन्दी भी इनसे कुछ भिन्न है। विचित्र किन्तु सत्य की इस पर भी मेरे मन में यह प्रश्न न उठा कि मैं इन लोगों की टोली का सदस्य कैसे बन गया हूँ ? विन्ध्याचल में ही मेरे लिए यह स्पष्ट हुआ कि जिन लोगों के साथ मैं चल रहा हूँ उनमें से किसका नाम क्या है ? तब तक वे सब मानो मेरे लिए एक ही थे। अब मैं समझ पाया कि बाबा धरमदास गुरु महाराज हैं। लोकदास उनके सबसे ज्ञानी चेले हैं, जड़ी-बूटियों और वैद्यक की अच्छी जानकारी रखते हैं। निर्बल और मन्दबुद्धि प्रीतमदास उनकी सबसे अधिक लगन से सेवा करते हैं। निक्कू उम्र में सबसे छोटे हैं ओर धरमदास उनके गुरु नहीं, गुरुभाई हैं। उन्हें ब्रह्मचारी या बजरबट्टू भी पुकारा जाता है। मेरा कोई नाम नहीं है।
बाबाजी धरमदास मुझे प्रायः बच्चा या पुत्तर कहकर पुकारते हैं। मुझे कभी-कभी बोबा कहकर भी सम्बोधित किया जाता है जिसका अर्थ गूँगा किंवा मूढ़ होता है इन लोगों की भाषा पंजाबी में। बाबा धरमदास कभी-कभी बड़े प्रेम से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे ‘ओय सदवस्तु।’ कहकर भी सम्बोधित कर डालते। सद् का तो पता नहीं वस्तु तो निश्चय ही रहा था। मैं बनारस पहुँचने तक। वहाँ मेरे वस्तु से धीरे-धीरे फिर व्यक्ति बनने का जो क्रम शुरू हुआ था वह विन्ध्याचल पहुँचकर जोर पकड़ने लगा। मेरा अतीत विन्ध्याचलवासिनी मंदिर में बाबाजी ने निक्कू को संन्यासदीक्षा दी। नूतन नाम दिया-दरसनदास।
उसने नागा बनना स्वीकार नहीं किया, वस्त्रधारी उदासीन बना वह। उसकी दिक्षा के बाद हम फिर निकल पड़े। हमारा गन्तव्य था कश्मीर किन्तु हमें वहाँ पहुँचने की कोई जल्दी न थी। चित्रकूट, प्रयाग, हरिद्वार और कांगड़ा होते हुए पहुँचे चार वर्ष में। बीच-बीच में जहाँ भी पड़ाव किया वहीं धूनी रमाए रहे महीनों तक। पंजाबी साधुओं के साथ रहते-रहते अब मैं भी उनकी-जैसी सधुक्कड़ी बोलने लगा। कद-काठी, गोरे रंग, भूरे सुनहरे केश और कंजी आँखों के कारण भी पंजाबी ही लगता था मैं। पूरी तरह उस टोली से एकात्म हो गया। साधुओं का वह परिवार ही अपना परिवार बन गया मेरे लिए।
वे सभी जन मेरे प्रति ऐसा व्यवहार करते थे मानो मैं लम्बी बीमारी से उठा उनका अबोध छोटा भाई होऊँ। धरमदास जी मुझे आध्यात्मिक शिक्षा देते, प्रीतमदासजी भजन गाना सिखाते, लोकदासजी जंगल में उगी जड़ी-बूटियाँ पहचानने और उनसे औषधियाँ बनाने की विधि बताते। और दरसन ? वह तो समवयस्क होने के कारण गुरु ही नहीं, मित्र की भूमिका में भी प्रस्तुत हो रहा था मेरे लिए। तो मैं भी अपने को बाबा धरमदास का चेला मानने लगा। उन साधुओं ने भी न इस घटना के बाद और न पहले कभी मुझसे यह पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ के हो ? और न स्वयं ही कुछ बताया इस बारे में।
मैं कहाँ आ गया हूँ। सुनकर उन साधुओं के चेहरे चमक उठे सुख-सन्तोष से। मैं दुहराता गया अपना प्रश्न। तब एक साधु ने ओठों पर अँगुली रखकर मुझे चुप रहने का निर्देश दिया। साधुओं ने आपस में बातें कीं अपनी भाषा में और उसी में मुझसे कुछ पूछा भी। ना, यह कथन तो भ्रामक है भयंकर रूप से। मुझे तब यह बोध न था कि मैं एक भाषा में बोला था और वे दूसरी बोल रहे हैं और ये भाषाएँ क्रमशः बांग्ला और हिन्दी कहलाती हैं। मेरी संज्ञा लौट आई थी किन्तु भेद-बुद्धि नहीं। सब कुछ एक समान था मेरे लिए। आकाश और पाताल, जड़ और चेतन, स्त्री और पुरुष, श्वेत और श्याम, गृहस्थ और साधु, किसी में भी कोई अन्तर नहीं कर पा रहा था मैं तब।
संज्ञा लौट आने के अनेक मास बाद तक भी यही स्थिति रही मेरी। मुझे कोई अन्तर न लगा उन साधुओं और अपने में, उनकी भाषा में और अपनी भाषा में। भाषा की कोई आवश्यकता न थी मेरे लिए। कुछ था ही नहीं बताने-पूछने को। ‘आमि कोथाय एलाम ?’ का वह प्रश्न पूछना भी छोड़ दिया मैंने। नवजात शिशु के स्तर पर ही पहुँच पाई थी तब तक मेरी चेतना। ना, नवजात शिशु भी उतना गूँगा-बहरा और अपने आस-पास को स्मृति में अंकित कर सकने में उतना असमर्थ नहीं होता जितना कि मैं था तब। मात्र इसी अर्थ में शिशु सिद्ध न हुआ मैं कि कुछ ही दिनों में उठने-बैठने, चलने-फिरने लगा। शिशु को तो प्रायः वर्ष-डेढ़ वर्ष लग जाते हैं।
‘कुछ ही दिनों’ की यह कथा भी सुनी मात्र सुनी-सुनाई है। काल के मुँह में पहुँचने की प्रक्रिया में अपना कालबोध भी गँवा बैठा था मैं। तो समय की सुइयाँ चलती रहीं, मैं भी चलता रहा साधुओं के साथ यन्त्रवत्, दिवस-मास बीतते गये, बदलता गया परिवेश। किन्तु मुझे इसका कोई ज्ञान न हुआ। वयोवृद्ध साधु मुझे बच्चा कहकर सम्बोधित करते रहे। पालते रहे मुझ असहाय को किसी सदय माँ की भाँति। वही मुझे औषधि देते, खाना खिलाते, शौच और स्नान कराते। वे जैसा कहते, मैं करता जाता। जैसे मेरी कोई अपनी इच्छा ही शेष न रह गई हो। सुनने में आपको विचित्र लगेगा किन्तु यह सत्य है कि बनारस पहुँचने तक मुझे यह भी चेतना न थी कि मैं मनुष्य हूँ कि पशु कि पाषाण कि पक्षी ?
मैं अपना ही नहीं, सभी प्राणियों, पदार्थों का नाम भूल चुका था। बनारस हम कब पहुँच गए, कैसे पहुँच गए इसका भी कोई भान न हो सका मुझे। बनारस पहुँचकर मन्द-मन्थर गति से लौटी चेतना। समझ पाया अन्ततः कि राँड़-साँड सीढ़ी संन्यासी भिन्न है एक-दूसरे से।
लेकिन इतनी चेतना नहीं लौटी कि समझ सकूँ कि मुझमें और मेरे साथियों में कोई विशेष अन्तर है। काशी में हमने एक मठ में डेरा किया। नगर में प्रवासी बंगालियों की काफी बड़ी आबादी होने के कारण मुझे बांग्ला बहुत सुनने को मिलने लगी। मुझे वह अतिपरिचित भाषा लगी और मैंने यह पाया कि स्वयं भी उसे बोल पाता हूँ, किन्तु मेरे मन में यह बात बिल्कुल नहीं उठी कि मैं बंगाली हूँ और बांग्ला मेरी मातृभाषा है। दो बंगाली साधुओं ने मुझसे बात की और जानना चाहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ। मैं जानता होता तब न बताता। मेरे तन भले ही साधुओं की जड़ी-बूटियों के चमत्कार से स्वस्थ होता चला गया हो, मन अब भी अस्वस्थ ही चल रहा था कदाचित्। ऐसा मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं अपनी स्मृति खो बैठा था बल्कि इसलिए कि अपनी खोई स्मृति खोजने की कोई उत्कण्ठा न थी मेरे मन में।
मैं घाट पर अपने साथ के बाबाजी और अन्य साधु सन्तों के प्रवचन सुनता रहता किन्तु वे भी मेरे शिथिल मन में कोई स्फूर्ति जगा न पाते। मैं पथराई आँखों से इधर-उधर देखता रहता और कभी-कभी पाता कि कुछ जोड़ा अन्य आँखों भी मुझे देख रही हैं बहुत विस्मय से। मानो प्रयास कर रही हों मुझे पहचानने का। बहुधा मुझे भी अपने को इसी प्रकार घूरने वाला व्यक्ति परिचित-सा प्रतीत होता। एक दिन हम लोग घाट पर बैठे हुए थे कि किसी परिचित-से लगते अपरिचित ने दूर से मुझे बड़े कुतूहल से देखा। फिर वह मेरे पास आया और उसकी आँखों में विस्मय का भाव गहराता गया। उसने मुझसे कहा बांग्ला में आप और इस भेस में ? मैं कुछ समझा नहीं। कह दिया कि साधु तो साधु के भेस में ही होगा। बोला, ‘जान सकता हूँ कि आप साधु बनने से पहले कौन थे, कहाँ थे ?’ मैं साधु बनने का रहस्य समझ नहीं पाया। पूछा, ‘आप क्या कहना चाहते हैं ?’ उसने प्रश्न फिर दुहराया लेकिन मेरा उत्तर तो वही हो सकता था जो पहले दे चुका था। तो वह जाकर हमारी टोली के मुखिया से बात करने लगा। उसी रात हमने बनारस से प्रस्थान कर दिया। विन्ध्याचल पहुँचकर धूनी रमाई। वहीं विन्ध्यवासिनी देवी की अनुकम्पा से मेरी चेतना लगभग भाषाहीन बच्चे से कुछ ऊपर उठी।
मैं पहली बार समझ पाया कि जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ उनसे भिन्न हूँ। वे उदासीन पन्थ के साधु हैं जबकि मैं नहीं हूँ। वे पंजाबी हैं और मैं कदाचित् बंगाली हूँ क्योंकि बांग्ला मुझे अच्छी तरह समझ में आती है जबकि इन लोगों की पंजाबी नहीं। मैं इनकी तरह हिन्दी बोल लेता हूँ लेकिन मेरी हिन्दी भी इनसे कुछ भिन्न है। विचित्र किन्तु सत्य की इस पर भी मेरे मन में यह प्रश्न न उठा कि मैं इन लोगों की टोली का सदस्य कैसे बन गया हूँ ? विन्ध्याचल में ही मेरे लिए यह स्पष्ट हुआ कि जिन लोगों के साथ मैं चल रहा हूँ उनमें से किसका नाम क्या है ? तब तक वे सब मानो मेरे लिए एक ही थे। अब मैं समझ पाया कि बाबा धरमदास गुरु महाराज हैं। लोकदास उनके सबसे ज्ञानी चेले हैं, जड़ी-बूटियों और वैद्यक की अच्छी जानकारी रखते हैं। निर्बल और मन्दबुद्धि प्रीतमदास उनकी सबसे अधिक लगन से सेवा करते हैं। निक्कू उम्र में सबसे छोटे हैं ओर धरमदास उनके गुरु नहीं, गुरुभाई हैं। उन्हें ब्रह्मचारी या बजरबट्टू भी पुकारा जाता है। मेरा कोई नाम नहीं है।
बाबाजी धरमदास मुझे प्रायः बच्चा या पुत्तर कहकर पुकारते हैं। मुझे कभी-कभी बोबा कहकर भी सम्बोधित किया जाता है जिसका अर्थ गूँगा किंवा मूढ़ होता है इन लोगों की भाषा पंजाबी में। बाबा धरमदास कभी-कभी बड़े प्रेम से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे ‘ओय सदवस्तु।’ कहकर भी सम्बोधित कर डालते। सद् का तो पता नहीं वस्तु तो निश्चय ही रहा था। मैं बनारस पहुँचने तक। वहाँ मेरे वस्तु से धीरे-धीरे फिर व्यक्ति बनने का जो क्रम शुरू हुआ था वह विन्ध्याचल पहुँचकर जोर पकड़ने लगा। मेरा अतीत विन्ध्याचलवासिनी मंदिर में बाबाजी ने निक्कू को संन्यासदीक्षा दी। नूतन नाम दिया-दरसनदास।
उसने नागा बनना स्वीकार नहीं किया, वस्त्रधारी उदासीन बना वह। उसकी दिक्षा के बाद हम फिर निकल पड़े। हमारा गन्तव्य था कश्मीर किन्तु हमें वहाँ पहुँचने की कोई जल्दी न थी। चित्रकूट, प्रयाग, हरिद्वार और कांगड़ा होते हुए पहुँचे चार वर्ष में। बीच-बीच में जहाँ भी पड़ाव किया वहीं धूनी रमाए रहे महीनों तक। पंजाबी साधुओं के साथ रहते-रहते अब मैं भी उनकी-जैसी सधुक्कड़ी बोलने लगा। कद-काठी, गोरे रंग, भूरे सुनहरे केश और कंजी आँखों के कारण भी पंजाबी ही लगता था मैं। पूरी तरह उस टोली से एकात्म हो गया। साधुओं का वह परिवार ही अपना परिवार बन गया मेरे लिए।
वे सभी जन मेरे प्रति ऐसा व्यवहार करते थे मानो मैं लम्बी बीमारी से उठा उनका अबोध छोटा भाई होऊँ। धरमदास जी मुझे आध्यात्मिक शिक्षा देते, प्रीतमदासजी भजन गाना सिखाते, लोकदासजी जंगल में उगी जड़ी-बूटियाँ पहचानने और उनसे औषधियाँ बनाने की विधि बताते। और दरसन ? वह तो समवयस्क होने के कारण गुरु ही नहीं, मित्र की भूमिका में भी प्रस्तुत हो रहा था मेरे लिए। तो मैं भी अपने को बाबा धरमदास का चेला मानने लगा। उन साधुओं ने भी न इस घटना के बाद और न पहले कभी मुझसे यह पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ के हो ? और न स्वयं ही कुछ बताया इस बारे में।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book