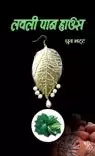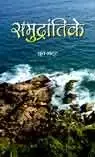|
सांस्कृतिक >> तत्त्वमसि तत्त्वमसिध्रुवभट्ट
|
171 पाठक हैं |
||||||
ध्रुवभट्ट का यह उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
अनुवादक की ओर से
लगभग तीन वर्ष पूर्व ‘तत्त्वमसि’ के विषय में प्रवीण
से सुना था। प्रवीण का सुझाव था कि अगर रुचे तो यह पुस्तक ऐसी है जो
हिन्दी में अनूदित होनी चाहिए।
‘तत्त्वमसि’ पढ़ने के कुछ समय पूर्व ही निर्मल वर्मा का ‘अंतिम अरण्य’ उपन्यास पढ़ा था। हालाँकि दोनों उपन्यास काफी अलग हैं, पर फिर भी दोनों में बहुत समान सूत्र भी हैं। हमें ऐसा लगा कि दो भाषाओं के, दो भिन्न साहित्यिक परंपराओं के, एक ही समय में रचनारत, एक ही तरह के सवालों से जूझते विभिन्न उम्र के ये दोनों लेखक एक जैसी ही भाषा बोलते हैं या बोलते हुए लगते हैं; इस बात को भारतीय पाठकों के सामने केवल अनुवाद के जरिए ही लाया जा सकता है।
मित्रों का सुझाव था कि श्री ध्रुव भट्ट की एक अन्य कृति ‘समुद्रान्तिके’ का अनुवाद मुझे करना चाहिए। मैंने दोनों पुस्तकें पढ़ीं। ‘तत्त्वमसि’ के प्रति मेरा झुकाव यथावत् रहा। उसी दौरान लेखक की एक अन्य कृति ‘अत्रापि’ भी लगभग लिखी जा चुकी थी। अब तो वह प्रकाशित भी हो गयी है।
‘तत्त्वमसि’ की कथा तो इस अनुवाद को पढ़कर आप जान ही जाएँगे। इसके अनेक पहलू आकृष्ट करते हैं। पर मुझे जिस बात ने सर्वाधिक आकृष्ट किया, वह है-मनुष्य को संसाधन मानता इस उपन्यास का नायक किस तरह जीवन की प्रक्रिया से गुजरते हुए मानव को जीता-जागता, हाड़-मांस का मनुष्य मानने लगता है।
हिन्दी के आलोचकों ने ‘अंतिम अरण्य’ में निर्मल वर्मा का हिन्दूवाद के प्रति झुकाव देखा था; गुजराती के हिन्दूवाद समर्थक आलोचकों को भी ‘तत्त्वमसि’ में ऐसा लगा। रूपवादियों को ‘समुद्रान्तिके’ ज़्यादा समर्थ रचना लगती है।
किन्तु हिन्दूवाद और रुपवाद के पार इसमें ‘निरे मनुष्य’, उसके परिवेश, उसके दुःख-सुख और उसके श्रम की बात है। बल्कि इस बहाने हमारी सांस्कृतिक पहचान को दृढ़ीभूत करनेवाली एक ऐसी गाथा है जिसका कहा जाना आज के समय में बहुत महत्त्वपूर्ण और ज़रूरी लगता है। आज ‘अतिवाद’ हमारे सामने सबसे बड़ा ख़तरा है-चाहे विचारधारा अतिवाद हो या धार्मिक/राजनौतिक हो।
शायद इसीलिए इसका अनुवाद मुझे ज़रूरी लगा। यह कृति मनुष्य जीवन और संस्कृति को अपने तरीके से व्याख्यायित करती है। गुजराती भाषा के कई स्तर इस कृति में उजागर होते हैं। बोलचाल की गुजराती, लोकबोली, तत्समप्रधान भाषा...और एक ऐसी चित्रात्मकता कि आपके सामने एक के बाद एक, दृश्य पर दृश्य सब घटित होता जाता है, जैसे लेखक विज़ुअल (दृश्य) टेकनीक का सहारा ले रहा हो। नर्मदा नायक की कथा बाँचती है, नायक आदिवासियों की कहानी कह रहा है, आदिवासी जंगलों की बात करते हैं...बड़े ही कौशल के साथ प्रस्तुत यह कृति अपनी शैली और कथ्य दोनों ही दृष्टियों से सही अर्थों में एक भारतीय उपन्यास है। नानी माँ की कथा, बिन्ता की कथा, कालेवाली माई की परंपरा, पुरिया की कहानी, जंगल की आग, जंगल की बारिश, जंगल की चुप्पी, जंगल का शोर, जंगल के दिन और जंगल की रातें...मिलकर एक ऐसा पोत रचते हैं कि यह कहना थोड़ा कठिन है कि इसमें कलात्मकता कम है।
अनुवाद की दृष्टि से कुछ समस्याएँ मेरी भी सामने आयीं। मैं कुछेक का ज़िक्र करना चाहूँगी। गुजराती में एक शब्द मुखरू है-जिसका शब्दकोशीय अर्थ सलेटी रंग होता है। मैंने संदर्भ के अनुसार कहीं सलेटी, कहीं मटमैला, कहीं बदरंग और कहीं सुनहरा भी इस्तेमाल किया है।
उसी तरह मकान के अलग-अलग हिस्सों के लिए परसाळ, ओटलो, डेलो, वाडो आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्थापत्य की दृष्टि से गुजराती मकानों के उन भागों के हिन्दी में सही पर्याय नहीं मिलते। अतः मुझे बरामदा, चबूतरा घूम-फिरकर बार-बार इस्तेमाल करने पड़े हैं। कुछ चीज़ों को फुटनोट में दिया है। कई जगहों पर अर्थ सुरक्षित रखते हुए वाक्य रचनाएँ बदली हैं। पर अनुवाद की ये वो सीमाएँ हैं जिनसे हर अनुवादक उलझता है। मेरा प्रयास रहा है कि हिन्दी के पाठकों को यह ‘निरा’ अनुवाद न लगे और ‘हिन्दी की प्रकृति के अधिक निकट लगे। कह नहीं सकती कि इसमें मुझे कितनी सफलता मिली है।
तीन वर्ष पूर्व ही श्री अशोक महेश्वरी जी से मेरा मौखिक अनुबन्ध हो चुका था कि वे इसका अनुवाद प्रकाशित करेंगे। भूकंप और दंगों की घटनाएँ नहीं हुई होतीं तो केन्द्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार की घोषणा से पूर्व इसका अनुवाद आप पढ़ चुके होते।
मैं सबसे पहले श्री ध्रुव भट्ट जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपनी पुस्तक का अनुवाद करने की अनुमति दी। इस अनुवाद प्रक्रिया में अपने जीवन-साथी प्रवीण को शामिल पाती हूँ।
मित्र बारिन मेहता से सर्वप्रथम ‘तत्त्वमसि’ पुस्तक उपलब्ध हुई, सो उनकी भी आभारी हूँ। साथ ही अख्तर ख़ान पठान और साथी अध्यापक-मित्र श्री अनिल भाई दवे के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने कम्प्यूटर टाइपिंग के प्रूफ देखने में ही मदद नहीं की बल्कि जो इस पूरी अनुवाद प्रक्रिया का हिस्सा भी बने मौलि, साकेत और शीतल का स्मरण भी सहज है, जिनका इसमें महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा।
इसका एक अंश ‘समकालीन भारतीय साहित्य’ में प्रकाशित करने के लिए मैं श्री गिरधर राठी की भी आभारी हूँ।
आशा है हिन्दी पाठकों को यह अनुवाद पसन्द आएगा।
‘तत्त्वमसि’ पढ़ने के कुछ समय पूर्व ही निर्मल वर्मा का ‘अंतिम अरण्य’ उपन्यास पढ़ा था। हालाँकि दोनों उपन्यास काफी अलग हैं, पर फिर भी दोनों में बहुत समान सूत्र भी हैं। हमें ऐसा लगा कि दो भाषाओं के, दो भिन्न साहित्यिक परंपराओं के, एक ही समय में रचनारत, एक ही तरह के सवालों से जूझते विभिन्न उम्र के ये दोनों लेखक एक जैसी ही भाषा बोलते हैं या बोलते हुए लगते हैं; इस बात को भारतीय पाठकों के सामने केवल अनुवाद के जरिए ही लाया जा सकता है।
मित्रों का सुझाव था कि श्री ध्रुव भट्ट की एक अन्य कृति ‘समुद्रान्तिके’ का अनुवाद मुझे करना चाहिए। मैंने दोनों पुस्तकें पढ़ीं। ‘तत्त्वमसि’ के प्रति मेरा झुकाव यथावत् रहा। उसी दौरान लेखक की एक अन्य कृति ‘अत्रापि’ भी लगभग लिखी जा चुकी थी। अब तो वह प्रकाशित भी हो गयी है।
‘तत्त्वमसि’ की कथा तो इस अनुवाद को पढ़कर आप जान ही जाएँगे। इसके अनेक पहलू आकृष्ट करते हैं। पर मुझे जिस बात ने सर्वाधिक आकृष्ट किया, वह है-मनुष्य को संसाधन मानता इस उपन्यास का नायक किस तरह जीवन की प्रक्रिया से गुजरते हुए मानव को जीता-जागता, हाड़-मांस का मनुष्य मानने लगता है।
हिन्दी के आलोचकों ने ‘अंतिम अरण्य’ में निर्मल वर्मा का हिन्दूवाद के प्रति झुकाव देखा था; गुजराती के हिन्दूवाद समर्थक आलोचकों को भी ‘तत्त्वमसि’ में ऐसा लगा। रूपवादियों को ‘समुद्रान्तिके’ ज़्यादा समर्थ रचना लगती है।
किन्तु हिन्दूवाद और रुपवाद के पार इसमें ‘निरे मनुष्य’, उसके परिवेश, उसके दुःख-सुख और उसके श्रम की बात है। बल्कि इस बहाने हमारी सांस्कृतिक पहचान को दृढ़ीभूत करनेवाली एक ऐसी गाथा है जिसका कहा जाना आज के समय में बहुत महत्त्वपूर्ण और ज़रूरी लगता है। आज ‘अतिवाद’ हमारे सामने सबसे बड़ा ख़तरा है-चाहे विचारधारा अतिवाद हो या धार्मिक/राजनौतिक हो।
शायद इसीलिए इसका अनुवाद मुझे ज़रूरी लगा। यह कृति मनुष्य जीवन और संस्कृति को अपने तरीके से व्याख्यायित करती है। गुजराती भाषा के कई स्तर इस कृति में उजागर होते हैं। बोलचाल की गुजराती, लोकबोली, तत्समप्रधान भाषा...और एक ऐसी चित्रात्मकता कि आपके सामने एक के बाद एक, दृश्य पर दृश्य सब घटित होता जाता है, जैसे लेखक विज़ुअल (दृश्य) टेकनीक का सहारा ले रहा हो। नर्मदा नायक की कथा बाँचती है, नायक आदिवासियों की कहानी कह रहा है, आदिवासी जंगलों की बात करते हैं...बड़े ही कौशल के साथ प्रस्तुत यह कृति अपनी शैली और कथ्य दोनों ही दृष्टियों से सही अर्थों में एक भारतीय उपन्यास है। नानी माँ की कथा, बिन्ता की कथा, कालेवाली माई की परंपरा, पुरिया की कहानी, जंगल की आग, जंगल की बारिश, जंगल की चुप्पी, जंगल का शोर, जंगल के दिन और जंगल की रातें...मिलकर एक ऐसा पोत रचते हैं कि यह कहना थोड़ा कठिन है कि इसमें कलात्मकता कम है।
अनुवाद की दृष्टि से कुछ समस्याएँ मेरी भी सामने आयीं। मैं कुछेक का ज़िक्र करना चाहूँगी। गुजराती में एक शब्द मुखरू है-जिसका शब्दकोशीय अर्थ सलेटी रंग होता है। मैंने संदर्भ के अनुसार कहीं सलेटी, कहीं मटमैला, कहीं बदरंग और कहीं सुनहरा भी इस्तेमाल किया है।
उसी तरह मकान के अलग-अलग हिस्सों के लिए परसाळ, ओटलो, डेलो, वाडो आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्थापत्य की दृष्टि से गुजराती मकानों के उन भागों के हिन्दी में सही पर्याय नहीं मिलते। अतः मुझे बरामदा, चबूतरा घूम-फिरकर बार-बार इस्तेमाल करने पड़े हैं। कुछ चीज़ों को फुटनोट में दिया है। कई जगहों पर अर्थ सुरक्षित रखते हुए वाक्य रचनाएँ बदली हैं। पर अनुवाद की ये वो सीमाएँ हैं जिनसे हर अनुवादक उलझता है। मेरा प्रयास रहा है कि हिन्दी के पाठकों को यह ‘निरा’ अनुवाद न लगे और ‘हिन्दी की प्रकृति के अधिक निकट लगे। कह नहीं सकती कि इसमें मुझे कितनी सफलता मिली है।
तीन वर्ष पूर्व ही श्री अशोक महेश्वरी जी से मेरा मौखिक अनुबन्ध हो चुका था कि वे इसका अनुवाद प्रकाशित करेंगे। भूकंप और दंगों की घटनाएँ नहीं हुई होतीं तो केन्द्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार की घोषणा से पूर्व इसका अनुवाद आप पढ़ चुके होते।
मैं सबसे पहले श्री ध्रुव भट्ट जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपनी पुस्तक का अनुवाद करने की अनुमति दी। इस अनुवाद प्रक्रिया में अपने जीवन-साथी प्रवीण को शामिल पाती हूँ।
मित्र बारिन मेहता से सर्वप्रथम ‘तत्त्वमसि’ पुस्तक उपलब्ध हुई, सो उनकी भी आभारी हूँ। साथ ही अख्तर ख़ान पठान और साथी अध्यापक-मित्र श्री अनिल भाई दवे के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने कम्प्यूटर टाइपिंग के प्रूफ देखने में ही मदद नहीं की बल्कि जो इस पूरी अनुवाद प्रक्रिया का हिस्सा भी बने मौलि, साकेत और शीतल का स्मरण भी सहज है, जिनका इसमें महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा।
इसका एक अंश ‘समकालीन भारतीय साहित्य’ में प्रकाशित करने के लिए मैं श्री गिरधर राठी की भी आभारी हूँ।
आशा है हिन्दी पाठकों को यह अनुवाद पसन्द आएगा।
-रंजना अरगड़े
इस लेखन के विषय में.....
नदियों में नर्मदा मुझे सर्वाधिक प्रिय है। इस लेखन में अपनी कल्पनाओं के
अतिरिक्त परिक्रमावासियों, नर्मदा तट पर रहनेवाले ग्रामजनों,
मंदिर-निवासियों, आश्रयवासियों के द्वारा सुनी हुई बातें और मेरे अपने
तट-भ्रमण के दौरान मुझे जिन बातों का पता चला उनका समावेश मैंने किया है।
साठसाली की बात पश्चिम अफ्रीका की डॉगॉन नाम की आदिवासी जाति की मान्यताओं
पर आधारित है।
इस देश को, उसकी परम सौंदर्यमयी प्रकृति को और उसके लोगों को मैं बेहद प्यार करता हूँ। मेरी जितनी इच्छा है उतना तो उसका दर्शन अटन मैं नहीं कर सका हूँ। जितना घूमा हूँ, उतने भर में भी मुझे मनुष्य-मनुष्य में जीवन के अलग-अलग अर्थ मिले हैं। अन्य देश देश तो मैंने देखे नहीं हैं। देखे होते तो वहाँ भी एसे ही अनुभव होते ऐसा विश्वास कहीं गहरे में पड़ा है।
किशोरावस्था से दो प्रश्न मुझे उलझाते रहे हैं :
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग कभी स्कूल में या गुरु के पास नहीं गए हैं उन्होंने ही भारतीय ज्ञान के आधारभूत माने जाने वाले लेखन के लिए सर्जनात्मक ऊर्जा प्रदान की है और साथ ही उसे बनाये रखने की वृहत्तर ज़िम्मेदारी भी उन्हीं की रही है। अलग भाषा, अलग रीति-रिवाज़ अलग अर्थ और दूसरी अनेक भिन्नताओं के बीच भी इस देश की बहुरंगी प्रजा में ऐसा कुछ है जो हर मनुष्य में समान है। वह क्या है ? इसका जवाब मुझे कभी, कहीं तो मिलेगा.....शायद मेरा यही जिज्ञासा इस लेखन का निमित्त बनी हो।
इससे अधिक इस लेखन के बारे में न ही मुझे कुछ कहना है न किसी से कहलवाना है।
इस देश को, उसकी परम सौंदर्यमयी प्रकृति को और उसके लोगों को मैं बेहद प्यार करता हूँ। मेरी जितनी इच्छा है उतना तो उसका दर्शन अटन मैं नहीं कर सका हूँ। जितना घूमा हूँ, उतने भर में भी मुझे मनुष्य-मनुष्य में जीवन के अलग-अलग अर्थ मिले हैं। अन्य देश देश तो मैंने देखे नहीं हैं। देखे होते तो वहाँ भी एसे ही अनुभव होते ऐसा विश्वास कहीं गहरे में पड़ा है।
किशोरावस्था से दो प्रश्न मुझे उलझाते रहे हैं :
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग कभी स्कूल में या गुरु के पास नहीं गए हैं उन्होंने ही भारतीय ज्ञान के आधारभूत माने जाने वाले लेखन के लिए सर्जनात्मक ऊर्जा प्रदान की है और साथ ही उसे बनाये रखने की वृहत्तर ज़िम्मेदारी भी उन्हीं की रही है। अलग भाषा, अलग रीति-रिवाज़ अलग अर्थ और दूसरी अनेक भिन्नताओं के बीच भी इस देश की बहुरंगी प्रजा में ऐसा कुछ है जो हर मनुष्य में समान है। वह क्या है ? इसका जवाब मुझे कभी, कहीं तो मिलेगा.....शायद मेरा यही जिज्ञासा इस लेखन का निमित्त बनी हो।
इससे अधिक इस लेखन के बारे में न ही मुझे कुछ कहना है न किसी से कहलवाना है।
-ध्रुव
भट्ट
ऋण स्वीकार
मेरे इस लेखन को धारावाहिक रूप में प्रकाशित करने वाले नवनीत-समर्पण,
भारतीय विद्याभवन तथा श्री दीपक जोशी को मैं इस क्षण याद करता हूँ।
श्री महेन्द्र चोटलिया ने साथ बैठकर, चर्चा करके मेरे इस लेखन को बेहतर बनाने में इतना अधिक योगदान दिया है कि उनका समावेश सर्जन-प्रक्रिया में हो सकता है।
श्री नरेशभाई वेद व्यक्तिगत रुचि लेकर मुझे मार्गदर्शन देते रहे हैं। उनके सुझाव काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए हैं।
श्री अंजनी नरवणे, जिन्होंने मेरी पहली किताब ‘समुद्रान्तिके’ का मराठी अनुवाद किया है, उन्होंने इस लेखन को नवनीत-समर्पण में पढ़कर, पूना से पत्र लिखकर मुझे उपयोगी जानकारियाँ एवं सुझाव दिये हैं।
मेरे आत्मीय श्री रेखा मेहता, श्री जयंतभाई ओझा, श्री अशोकपुरी गोस्वामी मेरी कृतियाँ सुनकर मुझे प्रोत्साहन देते रहे हैं।
इस पुस्तक का मुख्यपृष्ठ तैयार करने के लिए फोटोग्राफर श्री सुरेश पारेख तथा अक्षरांकन करनेवाले श्री कनु पटेल का मैं सादर-स्मरण करता हूँ।
गूर्जन ग्रंथ रत्नाकार की ओर से श्री मनुभाई शाह तथा भगवती ऑफसेट की ओर से श्री रोहितभाई ने मेरी बहुत मदद की है।
कृति किसी एक का सृजन माना जाए इस बात से मैं सहमत नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को मिले जाने-अनजाने लोग, उसके काम को ऊर्जा देने वाली घटनाएँ तथा अनेक बातों के प्रभाव से कृति का पट बुना जाता है।
इस तरह यह लेखन भी एक सहकारी सर्जन है।
श्री महेन्द्र चोटलिया ने साथ बैठकर, चर्चा करके मेरे इस लेखन को बेहतर बनाने में इतना अधिक योगदान दिया है कि उनका समावेश सर्जन-प्रक्रिया में हो सकता है।
श्री नरेशभाई वेद व्यक्तिगत रुचि लेकर मुझे मार्गदर्शन देते रहे हैं। उनके सुझाव काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए हैं।
श्री अंजनी नरवणे, जिन्होंने मेरी पहली किताब ‘समुद्रान्तिके’ का मराठी अनुवाद किया है, उन्होंने इस लेखन को नवनीत-समर्पण में पढ़कर, पूना से पत्र लिखकर मुझे उपयोगी जानकारियाँ एवं सुझाव दिये हैं।
मेरे आत्मीय श्री रेखा मेहता, श्री जयंतभाई ओझा, श्री अशोकपुरी गोस्वामी मेरी कृतियाँ सुनकर मुझे प्रोत्साहन देते रहे हैं।
इस पुस्तक का मुख्यपृष्ठ तैयार करने के लिए फोटोग्राफर श्री सुरेश पारेख तथा अक्षरांकन करनेवाले श्री कनु पटेल का मैं सादर-स्मरण करता हूँ।
गूर्जन ग्रंथ रत्नाकार की ओर से श्री मनुभाई शाह तथा भगवती ऑफसेट की ओर से श्री रोहितभाई ने मेरी बहुत मदद की है।
कृति किसी एक का सृजन माना जाए इस बात से मैं सहमत नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को मिले जाने-अनजाने लोग, उसके काम को ऊर्जा देने वाली घटनाएँ तथा अनेक बातों के प्रभाव से कृति का पट बुना जाता है।
इस तरह यह लेखन भी एक सहकारी सर्जन है।
-ध्रुव
भट्ट
तत्त्वमसि
देखता हूँ तुम्हें लगातार
आर-पार हवा के अगोचर आयाम की मानिंद
फैलती जाती हो तुम
अनंत में।
दृश्य-अदृश्य तरंग लीला में
लहराकर-कटकर
सर्जित-विसर्जित होती हो
असंख्य रूप-स्वरूपों में देखता हूँ
पर पहचान नहीं पाता।
पलकों के पीछे खुलती अजान भूमि पर
शुभ्रतम पुष्पों और अभूतपूर्व आवाज़ों की
गूढ़ वनराजि में
पीछा करता हूँ तुम्हारा
दौड़ता हूँ, उड़ता हूं, तैरता हूँ।
होकर पाषाण खड़ा रहता हूँ
और किसी दिव्य पल में बिखर जाता हूँ रेत बनकर
उभरती हैं पाँवों की छाप,
महसूस होता धीमा नम भार पर पकड़ नहीं पाता एक भी बार
कण कण में खुलता है कथा का एक स्तर
और अक्षर-अक्षर में उछलता है वही तुम्हारा जल।
आर-पार हवा के अगोचर आयाम की मानिंद
फैलती जाती हो तुम
अनंत में।
दृश्य-अदृश्य तरंग लीला में
लहराकर-कटकर
सर्जित-विसर्जित होती हो
असंख्य रूप-स्वरूपों में देखता हूँ
पर पहचान नहीं पाता।
पलकों के पीछे खुलती अजान भूमि पर
शुभ्रतम पुष्पों और अभूतपूर्व आवाज़ों की
गूढ़ वनराजि में
पीछा करता हूँ तुम्हारा
दौड़ता हूँ, उड़ता हूं, तैरता हूँ।
होकर पाषाण खड़ा रहता हूँ
और किसी दिव्य पल में बिखर जाता हूँ रेत बनकर
उभरती हैं पाँवों की छाप,
महसूस होता धीमा नम भार पर पकड़ नहीं पाता एक भी बार
कण कण में खुलता है कथा का एक स्तर
और अक्षर-अक्षर में उछलता है वही तुम्हारा जल।
-महेन्द्र चोटलिया
ले, खा ले...
यह आवाज़ बहुत पास से सुनायी पड़ रही है। कोई बहुत पास बैठकर मुझसे कह रहा
है। मैं मानो गहरी निद्रा में से जाग रहा होऊँ या फिर तन्द्रा में होऊँ इस
तरह स्वर और शब्द, पहचानने का प्रयत्न करना पड़ रहा है।
‘‘ले, खा ले’’-ये धुंधले
शब्द-स्त्री स्वर हैं जो इस निर्जन वन में, निःशब्द टीलों पर झुके नीलातीत
आकाश के उस पार से आ रहे हैं, इतना ही जान पाया।
मैंने प्रयत्नपूर्वक आँखें खोलीं। रेतीले, पथरीले नदी तट पर वह मेरे दाहिने ओर बैठी थीं। लाल रंग के घाघरी-चोली में वह, घुटनों पर बैठी, मुझ पर झुकी हुई कह रही है ‘‘ले, खा ले’’। उसके नन्हें हाथों में मकई का भुट्टा था, जो उसने मेरे मुँह के आगे धरा था।’’
बड़ी मुश्किल से हाथ उठाकर, मैं वह भुट्टा लेता हूँ। धीरे-धीरे मेरी स्थगित चेतना जागृत होती है। धैर्यपूर्वक मक्के का एक दाना निकालकर मैं अपने मुँह में रखता हूँ।
कितनी देर से यहाँ पड़ा हूँ, याद नहीं। पर एक बात निःसंदेह याद है कि अभी जो ‘ले’ शब्द मेरे कानों में पड़ा, उसके पूर्व सुना हुआ अंतिम मनुष्य स्वर था-‘‘दे दे’’। मनुष्य भूखे पेट जितना रह सके उससे अधिक तो नहीं ही। फिर भी इन दोनों शब्दों को जोड़ने बैठूँ, तो समय अनंत बन जाता है। वर्षों सदियों, मन्वन्तरों के आरपार उसकी जड़े फैली हुईं दिखायी पड़ती हैं।
परंपरा, संस्कृति और समय की कड़ी के रूप में ये शब्द, अब केवल दो तीन शब्द-भर कहाँ रह गए हैं ? वे तो बन गए हैं भाष्य। अनादि काल से अघोर अरण्य, निर्जन पगडंडी और आदिम पत्थरों के पार वह रहे इस परम पारदर्शक जल की तरह ये दो शब्द सनातन कथा बनकर बह रहे हैं।
किनारे पर झुकी वनराजि, रंगबिरंगी गोट्टियाँ जैसे गोल पत्थरों से आवृत किनारा, और सृष्टि के समय से ही, मौन खड़े टीलों के बीच अविराम वह रहा यह निर्मल जल-इन सबकी साक्षी में-जिसका न आदि है न अंत, ऐसी किसी महाकथा की भाँति ये शब्द ‘‘दे दे’’ और ‘‘ले’’ अनादि अनंत बनकर बह रहे हैं।
मैंने भुट्टे पर से ध्यान हटाकर उस देनेवाली की ओर दृष्टि फेरी। कौन होगी वह वन कन्या ? बोलने की कोशिश करता हूँ, तो गला भर आता है। साथ ही साथ आँखें भी।
जल भरी आँखों की झिलमिली के पार हल्के-हल्के दृश्य दिखलायी पड़ रहे हैं। मानो सब कुछ पुनर्जीवित हो रहा हो, इस तरह सारा कुछ दुबारा घटित होता देख सकता हूँ। जीवन कितनी छोटी और सँकरी पगडंडी पर चला जा रहा है इसका अनुभव अनंत काल से बह रहे इस महाजल प्रवाह के पास पड़े-पड़े कर रहा हूँ।
दोनों शब्दों को जोड़ते हुए समय को लयबद्ध करने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे सब कुछ बस कल ही तो हुआ था, कुछ इस तरह आँखों के आगे आकर उपस्थित हो उठता है।
इतना पढ़कर डायरी बन्द कर देती हूँ और थोड़ी देर सोच में पड़ जाती हूँ। इस निर्जन पथरीले किनारे पर अपनी बची-खुची पूँजी रख रहा हो इस तरह थैली में लपेट कर यह डायरी, कुछ पत्र और तस्वीरें रखकर वह चल पड़ा। उसने जिसका त्याग किया उसे स्वीकर कर, सम्हालने की मुझे आज्ञा मिली है। ऋणानुबंध का कोई नाम नहीं होता। उसका तो होता है, केवल ऋण। परापूर्व से चली आती परंपरा की तरह यह ऋण मुझे निभाना है। इसी हेतु रोज़ सुबह यहाँ बैठकर ये डायरी, ये पत्र, फोटोग्राफ पढ़कर देखकर ‘दे दे’ और ‘ले’ के बीच के समय का एकाध तंतु जोड़ देने का प्रयास करूँगी।
उसने अपना नाम इस डायरी में कहीं नहीं लिखा है, न ही इन पत्रों में कहीं उसका नाम है। मैंने उसको देखा अवश्य है। वह छः सात साल का था और पुल पर से गुज़र रही ट्रेन की खिड़की में से झाँक रहा था, तब से मैं उसे पहचानती हूँ। बीच में कई वर्ष वह विदेश में रहा यह बात इस डायरी से पता चली। वह जब वापस लौटा तब सब कुछ पहले जैसा था-ट्रेन, खिड़की और उसकी जिज्ञासा आँखें-हाँ, उसकी मुखरेखा, बात करने के समझने के, उसके तरीके में मुझे काफ़ी फर्क लगा। एक क्षण तो मुझे ऐसा लगा कि देश वापस लौटना उसे अच्छा नहीं लगा है। पर वह सब छोड़िए-मुझे तो आपको ले जाना है एक अनजाने प्रदेश में :
‘‘....उस रात अठारह वर्षों बाद मैं इस देश में वापस लौट रहा था; किन्तु इतने लम्बे अन्तराल के बाद स्वदेश वापस लौटने वाले को जैसी अनुभूति होनी चाहिए वैसी मुझे नहीं हो रही थी। प्रोफ़ेसर रूडोल्फ ने जब आदिवासी संस्कृति के अध्ययन के लिए मेरा नाम सुझाया, तब मुझे अच्छा नहीं लगा था। कुछ अरुचि का भाव हो आया था। युनिवर्सिटी का जीवन या लूसी का साथ दोनों में से एक भी छोड़ पाना मेरे लिए सजा ही था। जंगल में जाकर रहना, कोई रुचिकर काम तो नहीं ही कहलाएगा।
वास्तव में तो यह प्रोजक्ट तुषार को सौंपा जाना चाहिए था। अगर अब भी उसे सौंप दिया जाए तो अच्छा होगा। ‘‘मुझसे नहीं होगा’’-मैंने तर्क करने की कोशिश की। बरसों से विदेश में बसे होने के बावजूद तुषार अन्दर से देश के प्रति आकर्षण, ललक और खिंचाव अनुभव करता है, यह मुझे मालूम था। मेरे मतानुसार ऐसा कुछ भी अनुभव करना निरी भावुकता के अलावा कुछ नहीं है मैं तो मानव संसाधन विकास का प्रखर समर्थक था। मनुष्य की खूबियाँ परख कर उनमें से महत्तम उत्पादकता सिद्ध करना-यही मेरा काम है। आदिजातियों के पीछे या अन्य किसी खोज के पीछे भटकने में कोई उत्पादकता सिद्ध होती हो, ऐसा मुझे नहीं लगता था। हाँ, लूसी को ज़रूर यह सब बहुत अच्छा लगता है। पर उसकी रुचि केवल इसी बात में थी कि या तो उसके लेख छपे या फिर-खोज के रोमांच का अनुभव हो। इससे अधिक कुछ नहीं।
‘‘होगा, तुमसे अवश्य होगा’’-प्रोफ़ेसर ने मेरा तर्क काटते हुए कहा था। ‘‘मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि मुझे तुम्हीं को भेजना है। तुषार को नहीं। तुम्हीं को ! ठीक है !’’
‘‘सर’’, मैंने यथासंभव नम्रतापूर्व कहा-‘‘आप ऐसा मानते हैं इसकी मुझे खुशी है। परन्तु जन्म से भारतीय होने पर भी मैं भारत में ज्यादा रहा नहीं हूँ। उसमें भी आदिवासी इलाके में तो कभी गया नहीं हूँ।’’
बूढ़े प्रोफ़ेसर ने अविश्वास के साथ मुझे देखा और सिर धुनते हुए कहा, ‘‘वो जो हो’। पर तुम जा रहे हो। तुम्हें चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुप्रिया भारतीय को सब समझा दिया है। तुम एक बार उसके पास पहुँच जाओ।’’
पिछले छः महीनों से भारत की किसी सुप्रिया भारतीय के पत्र आते थे। एकाध बार कम्प्यूटर फ्लॉपी भी आयी थी इतनी-सी बात से प्रोफ़ेसर रूडोल्फ चाहे सुप्रिया से प्रभावित हुए हों, पर मुझे बहुत उम्मीद न थी। आदिवासी कल्याण केन्द्र चलाने वाली सुप्रिया भारतीय यानी खादी के कपड़े पहने साठ पैंसठ वर्ष की चशमिश, स्वयंसेवकों से घिरी, गाँधीजी के नाम से भाषण देनेवाली स्त्री। मेरे मन में उनकी यही शोभनीय आकृति बनी हुई थी और इसकी सत्यता के बारे में मेरे मन में कोई सन्देह नहीं था। रूडोल्फ के मन को कोई चोट न पहुँचे यह सोचकर मैं चुप रहा। पर मैंने यह जरूर पूछा-‘सुप्रिया के साथ काम करना क्या जरूरी है ?’’
बिल्कुल नहीं ! तुम अपने ही ढंग से काम करना !’’ फिर खड़े होकर मेरे पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा-‘‘आदिवासियों के साथ घुलने-मिलने में सुप्रिया तुम्हारी मदद करेगी। एक बार तुम उनसे घुल मिल जाओ, वे सब तुम्हें अपना मानने लगें, उसके बाद ही तुम उनकी संस्कृति के बारे में जान सकोगे। तब तक तुम जानकारियाँ ही इकट्ठा कर पाओगे, अधिक कुछ नहीं। I want you to sit with them to have dialogues with them and to do participatory observations.’’
मेरे पास इसका कोई जवाब न था। मैंने जरा उलझन भरे स्वर में कहा-H.R.D. का काम होता तो मैं सरलता से कर पाता। यह विषय मेरे लिए एकदम नया है। मुझे तो पता भी नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करूँगा। क-ख-ग से ही शुरु करना पड़ेगा।’’
‘‘अरे ! वाह !’’ प्रोफ़ेसर एकदम ख़ुश होकर बोल पड़े। ‘‘सचमुच क ख ग से ही शुरु करो। तुम एक छोटी सी स्कूल खोलना और वहाँ रहना। तुम्हें वहाँ आदिवासियों के बीच रहना है, उनकी रोज़-बरोज़ की ज़िन्दगी को समझना है, उसे अपनी डायरी में लिखना है, और उसकी एक नकल मुझे भेजते रहना है। बस यही होगी तुम्हारी रिपोर्ट।’’ ऐसी अनगढ़ रिपोर्ट के लिए उस धुनी प्रोफ़ेसर ने युनिवर्सिटी से न जाने कितने सारे डॉलर का अनुदान मंज़ूर करवाया था।
प्रोफ़ेसर एक दो बार भारत आ चुके थे। यहाँ के अध्यापकों और विद्यार्थियों के बारे में क्या समझ ले कर लौट होंगे, यह तो मुझे नहीं मालूम; पर उन्हें भारतीय अध्यापकों और समाज के संबंधों के प्रति विशेष लगाव है, यह मुझे अच्छी तरह मालूम था।
खैर, नंगे भूखे आदिवासियों और किसी खादीधारिणी सुप्रिया भारतीय के बीच रह कर कुछ टिप्पणियाँ लिखकर भाग आना, बहुत मुश्किल न होगा। मेरे एकाध दो पत्र पाकर ही रुडोल्फ मुझे वापस बुला लेंगे।
सौभाग्य से तुषार मेरे साथ मुम्बई तक आया था। वह तो मुम्बई पहुँचते ही नाच उठा था। कहा-‘‘चलो यार, हम अपनी स्कूल देख आएँ।’’
‘‘स्टुपिड’’, मैंने कहा, ‘‘छोड़ो यार, फातलू की भावुकता। अगर तुम कहो तो जीवन जीने की कला पर दो भाषण दे डालूँ।’’
‘‘अरे भाई’’ तुषार ने नाटकीय अंदाज़ में कहा, ‘‘हम तो जैसे हैं भले हैं। आप पधारिए अपनी सुप्रिया जी के देश। चाहो तो आज रात की गाड़ी का ही टिकट कन्फर्म करा दूँगा।’’
और सचमुच तुषार ने ऐसा ही किया। रात को जब मुझे स्टेशन पर छोड़ने आया तो कहा-‘‘यार अगर हम इन्सान ही मिट जाएँ, तो क्या फायदा ? थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ, हम कुछ हैं। बस, इससे अधिक कुछ नहीं। मुझे तो सब कुछ याद आता है हमारी स्कूल, वह हमारी टीचर-सिस्टर एस्थर...सचमुच वे दिन भी क्या खूब थे।’’
कहते हुए उसका स्वर नम हो आया।
‘‘तुम किया करो उन दिनों को याद और बैठे रहो’’ मैंने कहा था, ‘‘और देखते रहना कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गयी है।’’
ट्रेन चली और वह गया। मुझे पूरा विश्वास था कि अभी इस समय रात के ग्यारह बजे भी वह स्कूल की बन्द इमारत के पास अपनी कार रोकेगा। कुछ देर वहाँ रुककर सिगरेट पिएगा। तब घर जाएगा।
जो हो सो ! तुषार का ख़याल परे हटाकर मैं ‘मानव विकास संसाधन की प्रयुक्तियाँ’ किताब पढ़ते हुए कब सो गया, पता भी न चला।
मैंने प्रयत्नपूर्वक आँखें खोलीं। रेतीले, पथरीले नदी तट पर वह मेरे दाहिने ओर बैठी थीं। लाल रंग के घाघरी-चोली में वह, घुटनों पर बैठी, मुझ पर झुकी हुई कह रही है ‘‘ले, खा ले’’। उसके नन्हें हाथों में मकई का भुट्टा था, जो उसने मेरे मुँह के आगे धरा था।’’
बड़ी मुश्किल से हाथ उठाकर, मैं वह भुट्टा लेता हूँ। धीरे-धीरे मेरी स्थगित चेतना जागृत होती है। धैर्यपूर्वक मक्के का एक दाना निकालकर मैं अपने मुँह में रखता हूँ।
कितनी देर से यहाँ पड़ा हूँ, याद नहीं। पर एक बात निःसंदेह याद है कि अभी जो ‘ले’ शब्द मेरे कानों में पड़ा, उसके पूर्व सुना हुआ अंतिम मनुष्य स्वर था-‘‘दे दे’’। मनुष्य भूखे पेट जितना रह सके उससे अधिक तो नहीं ही। फिर भी इन दोनों शब्दों को जोड़ने बैठूँ, तो समय अनंत बन जाता है। वर्षों सदियों, मन्वन्तरों के आरपार उसकी जड़े फैली हुईं दिखायी पड़ती हैं।
परंपरा, संस्कृति और समय की कड़ी के रूप में ये शब्द, अब केवल दो तीन शब्द-भर कहाँ रह गए हैं ? वे तो बन गए हैं भाष्य। अनादि काल से अघोर अरण्य, निर्जन पगडंडी और आदिम पत्थरों के पार वह रहे इस परम पारदर्शक जल की तरह ये दो शब्द सनातन कथा बनकर बह रहे हैं।
किनारे पर झुकी वनराजि, रंगबिरंगी गोट्टियाँ जैसे गोल पत्थरों से आवृत किनारा, और सृष्टि के समय से ही, मौन खड़े टीलों के बीच अविराम वह रहा यह निर्मल जल-इन सबकी साक्षी में-जिसका न आदि है न अंत, ऐसी किसी महाकथा की भाँति ये शब्द ‘‘दे दे’’ और ‘‘ले’’ अनादि अनंत बनकर बह रहे हैं।
मैंने भुट्टे पर से ध्यान हटाकर उस देनेवाली की ओर दृष्टि फेरी। कौन होगी वह वन कन्या ? बोलने की कोशिश करता हूँ, तो गला भर आता है। साथ ही साथ आँखें भी।
जल भरी आँखों की झिलमिली के पार हल्के-हल्के दृश्य दिखलायी पड़ रहे हैं। मानो सब कुछ पुनर्जीवित हो रहा हो, इस तरह सारा कुछ दुबारा घटित होता देख सकता हूँ। जीवन कितनी छोटी और सँकरी पगडंडी पर चला जा रहा है इसका अनुभव अनंत काल से बह रहे इस महाजल प्रवाह के पास पड़े-पड़े कर रहा हूँ।
दोनों शब्दों को जोड़ते हुए समय को लयबद्ध करने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे सब कुछ बस कल ही तो हुआ था, कुछ इस तरह आँखों के आगे आकर उपस्थित हो उठता है।
इतना पढ़कर डायरी बन्द कर देती हूँ और थोड़ी देर सोच में पड़ जाती हूँ। इस निर्जन पथरीले किनारे पर अपनी बची-खुची पूँजी रख रहा हो इस तरह थैली में लपेट कर यह डायरी, कुछ पत्र और तस्वीरें रखकर वह चल पड़ा। उसने जिसका त्याग किया उसे स्वीकर कर, सम्हालने की मुझे आज्ञा मिली है। ऋणानुबंध का कोई नाम नहीं होता। उसका तो होता है, केवल ऋण। परापूर्व से चली आती परंपरा की तरह यह ऋण मुझे निभाना है। इसी हेतु रोज़ सुबह यहाँ बैठकर ये डायरी, ये पत्र, फोटोग्राफ पढ़कर देखकर ‘दे दे’ और ‘ले’ के बीच के समय का एकाध तंतु जोड़ देने का प्रयास करूँगी।
उसने अपना नाम इस डायरी में कहीं नहीं लिखा है, न ही इन पत्रों में कहीं उसका नाम है। मैंने उसको देखा अवश्य है। वह छः सात साल का था और पुल पर से गुज़र रही ट्रेन की खिड़की में से झाँक रहा था, तब से मैं उसे पहचानती हूँ। बीच में कई वर्ष वह विदेश में रहा यह बात इस डायरी से पता चली। वह जब वापस लौटा तब सब कुछ पहले जैसा था-ट्रेन, खिड़की और उसकी जिज्ञासा आँखें-हाँ, उसकी मुखरेखा, बात करने के समझने के, उसके तरीके में मुझे काफ़ी फर्क लगा। एक क्षण तो मुझे ऐसा लगा कि देश वापस लौटना उसे अच्छा नहीं लगा है। पर वह सब छोड़िए-मुझे तो आपको ले जाना है एक अनजाने प्रदेश में :
‘‘....उस रात अठारह वर्षों बाद मैं इस देश में वापस लौट रहा था; किन्तु इतने लम्बे अन्तराल के बाद स्वदेश वापस लौटने वाले को जैसी अनुभूति होनी चाहिए वैसी मुझे नहीं हो रही थी। प्रोफ़ेसर रूडोल्फ ने जब आदिवासी संस्कृति के अध्ययन के लिए मेरा नाम सुझाया, तब मुझे अच्छा नहीं लगा था। कुछ अरुचि का भाव हो आया था। युनिवर्सिटी का जीवन या लूसी का साथ दोनों में से एक भी छोड़ पाना मेरे लिए सजा ही था। जंगल में जाकर रहना, कोई रुचिकर काम तो नहीं ही कहलाएगा।
वास्तव में तो यह प्रोजक्ट तुषार को सौंपा जाना चाहिए था। अगर अब भी उसे सौंप दिया जाए तो अच्छा होगा। ‘‘मुझसे नहीं होगा’’-मैंने तर्क करने की कोशिश की। बरसों से विदेश में बसे होने के बावजूद तुषार अन्दर से देश के प्रति आकर्षण, ललक और खिंचाव अनुभव करता है, यह मुझे मालूम था। मेरे मतानुसार ऐसा कुछ भी अनुभव करना निरी भावुकता के अलावा कुछ नहीं है मैं तो मानव संसाधन विकास का प्रखर समर्थक था। मनुष्य की खूबियाँ परख कर उनमें से महत्तम उत्पादकता सिद्ध करना-यही मेरा काम है। आदिजातियों के पीछे या अन्य किसी खोज के पीछे भटकने में कोई उत्पादकता सिद्ध होती हो, ऐसा मुझे नहीं लगता था। हाँ, लूसी को ज़रूर यह सब बहुत अच्छा लगता है। पर उसकी रुचि केवल इसी बात में थी कि या तो उसके लेख छपे या फिर-खोज के रोमांच का अनुभव हो। इससे अधिक कुछ नहीं।
‘‘होगा, तुमसे अवश्य होगा’’-प्रोफ़ेसर ने मेरा तर्क काटते हुए कहा था। ‘‘मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि मुझे तुम्हीं को भेजना है। तुषार को नहीं। तुम्हीं को ! ठीक है !’’
‘‘सर’’, मैंने यथासंभव नम्रतापूर्व कहा-‘‘आप ऐसा मानते हैं इसकी मुझे खुशी है। परन्तु जन्म से भारतीय होने पर भी मैं भारत में ज्यादा रहा नहीं हूँ। उसमें भी आदिवासी इलाके में तो कभी गया नहीं हूँ।’’
बूढ़े प्रोफ़ेसर ने अविश्वास के साथ मुझे देखा और सिर धुनते हुए कहा, ‘‘वो जो हो’। पर तुम जा रहे हो। तुम्हें चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुप्रिया भारतीय को सब समझा दिया है। तुम एक बार उसके पास पहुँच जाओ।’’
पिछले छः महीनों से भारत की किसी सुप्रिया भारतीय के पत्र आते थे। एकाध बार कम्प्यूटर फ्लॉपी भी आयी थी इतनी-सी बात से प्रोफ़ेसर रूडोल्फ चाहे सुप्रिया से प्रभावित हुए हों, पर मुझे बहुत उम्मीद न थी। आदिवासी कल्याण केन्द्र चलाने वाली सुप्रिया भारतीय यानी खादी के कपड़े पहने साठ पैंसठ वर्ष की चशमिश, स्वयंसेवकों से घिरी, गाँधीजी के नाम से भाषण देनेवाली स्त्री। मेरे मन में उनकी यही शोभनीय आकृति बनी हुई थी और इसकी सत्यता के बारे में मेरे मन में कोई सन्देह नहीं था। रूडोल्फ के मन को कोई चोट न पहुँचे यह सोचकर मैं चुप रहा। पर मैंने यह जरूर पूछा-‘सुप्रिया के साथ काम करना क्या जरूरी है ?’’
बिल्कुल नहीं ! तुम अपने ही ढंग से काम करना !’’ फिर खड़े होकर मेरे पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा-‘‘आदिवासियों के साथ घुलने-मिलने में सुप्रिया तुम्हारी मदद करेगी। एक बार तुम उनसे घुल मिल जाओ, वे सब तुम्हें अपना मानने लगें, उसके बाद ही तुम उनकी संस्कृति के बारे में जान सकोगे। तब तक तुम जानकारियाँ ही इकट्ठा कर पाओगे, अधिक कुछ नहीं। I want you to sit with them to have dialogues with them and to do participatory observations.’’
मेरे पास इसका कोई जवाब न था। मैंने जरा उलझन भरे स्वर में कहा-H.R.D. का काम होता तो मैं सरलता से कर पाता। यह विषय मेरे लिए एकदम नया है। मुझे तो पता भी नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करूँगा। क-ख-ग से ही शुरु करना पड़ेगा।’’
‘‘अरे ! वाह !’’ प्रोफ़ेसर एकदम ख़ुश होकर बोल पड़े। ‘‘सचमुच क ख ग से ही शुरु करो। तुम एक छोटी सी स्कूल खोलना और वहाँ रहना। तुम्हें वहाँ आदिवासियों के बीच रहना है, उनकी रोज़-बरोज़ की ज़िन्दगी को समझना है, उसे अपनी डायरी में लिखना है, और उसकी एक नकल मुझे भेजते रहना है। बस यही होगी तुम्हारी रिपोर्ट।’’ ऐसी अनगढ़ रिपोर्ट के लिए उस धुनी प्रोफ़ेसर ने युनिवर्सिटी से न जाने कितने सारे डॉलर का अनुदान मंज़ूर करवाया था।
प्रोफ़ेसर एक दो बार भारत आ चुके थे। यहाँ के अध्यापकों और विद्यार्थियों के बारे में क्या समझ ले कर लौट होंगे, यह तो मुझे नहीं मालूम; पर उन्हें भारतीय अध्यापकों और समाज के संबंधों के प्रति विशेष लगाव है, यह मुझे अच्छी तरह मालूम था।
खैर, नंगे भूखे आदिवासियों और किसी खादीधारिणी सुप्रिया भारतीय के बीच रह कर कुछ टिप्पणियाँ लिखकर भाग आना, बहुत मुश्किल न होगा। मेरे एकाध दो पत्र पाकर ही रुडोल्फ मुझे वापस बुला लेंगे।
सौभाग्य से तुषार मेरे साथ मुम्बई तक आया था। वह तो मुम्बई पहुँचते ही नाच उठा था। कहा-‘‘चलो यार, हम अपनी स्कूल देख आएँ।’’
‘‘स्टुपिड’’, मैंने कहा, ‘‘छोड़ो यार, फातलू की भावुकता। अगर तुम कहो तो जीवन जीने की कला पर दो भाषण दे डालूँ।’’
‘‘अरे भाई’’ तुषार ने नाटकीय अंदाज़ में कहा, ‘‘हम तो जैसे हैं भले हैं। आप पधारिए अपनी सुप्रिया जी के देश। चाहो तो आज रात की गाड़ी का ही टिकट कन्फर्म करा दूँगा।’’
और सचमुच तुषार ने ऐसा ही किया। रात को जब मुझे स्टेशन पर छोड़ने आया तो कहा-‘‘यार अगर हम इन्सान ही मिट जाएँ, तो क्या फायदा ? थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ, हम कुछ हैं। बस, इससे अधिक कुछ नहीं। मुझे तो सब कुछ याद आता है हमारी स्कूल, वह हमारी टीचर-सिस्टर एस्थर...सचमुच वे दिन भी क्या खूब थे।’’
कहते हुए उसका स्वर नम हो आया।
‘‘तुम किया करो उन दिनों को याद और बैठे रहो’’ मैंने कहा था, ‘‘और देखते रहना कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गयी है।’’
ट्रेन चली और वह गया। मुझे पूरा विश्वास था कि अभी इस समय रात के ग्यारह बजे भी वह स्कूल की बन्द इमारत के पास अपनी कार रोकेगा। कुछ देर वहाँ रुककर सिगरेट पिएगा। तब घर जाएगा।
जो हो सो ! तुषार का ख़याल परे हटाकर मैं ‘मानव विकास संसाधन की प्रयुक्तियाँ’ किताब पढ़ते हुए कब सो गया, पता भी न चला।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book