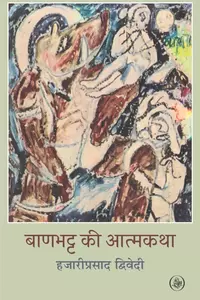|
लेख-निबंध >> आलोक पर्व आलोक पर्वहजारी प्रसाद द्विवेदी
|
384 पाठक हैं |
|||||||
इस पुस्तक में भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के स्वरूप पढ़ने को मिलते हैं...
Aalok Parva a hindi book by Hazari Prasad Dwivedi - आलोक पर्व - हजारीप्रसाद द्विवेदी
प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश
आचार्य द्विवेदी के ऐसे वाङ्मय-पुरुष हैं जिनका संस्कृत मुख है, प्राकृत बाहु है, अपभ्रंश जघन है और हिन्दी पाद है। आलोक पर्व के निबन्ध पढ़कर मन की आँखों के सामने उनका यह रूप साकार हो उठता है।
अन्धकार से जूझना है !
न जाने कब से मनुष्य के अन्तरतर से ‘दीन-रट’ निकलती रही, मैं अन्धकार से घिर गया हूँ, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो।-‘तमसो मा ज्योतिर्गमय !’ परन्तु यह पुकार शायद सुनी नहीं गई।-‘होत न श्याम सहाय !’ प्रकाश और अन्धकार की आँखमिचौनी चलती ही रही, चलती ही रहेगी। यह तो विधि-विधान है। कौन टाल सकता है इसे !
लेकिन मनुष्य के अन्तर्यामी निष्क्रिय नहीं हैं। वे थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते नहीं। वे अधीर भी नहीं होते। वैज्ञानिक का विश्वास है कि अनन्त रुपों में विकसित होते-होते वे मनुष्य के विवेक रूप में प्रत्यक्ष हुए हैं। करोड़ों वर्ष लगे हैं इस रूप में प्रकट होने में। उन्होंने धीरज नहीं छोड़ा। स्पर्शेन्द्रिय से स्वादेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय की और फिर चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रियेन्द्रिय की ओर अपने-आपको अभिव्यक्ति करते हुए मन और बुद्धि के रूप में आविर्भूत हुए हैं। और भी न जाने किन रूपों में अग्रसर हों। वैज्ञानिक को ‘अन्तर्यामी’ शब्द पसन्द नहीं है। कदाचित् वह प्राणशक्ति कहना पसन्द करे। नाम का क्या झगड़ा है ?
जीव का काम पुरा काल में स्पर्श से चल जाता था, बाद में उसने घ्राण शक्ति पाई। वह दूर-दूर की चीज़ों का अन्दाज़ा लगाने लगा। पहले स्पर्श से भिन्न सब कुछ अन्धकार था। अन्तर्यामी रुके नहीं। घ्राण का जगत्, फिर स्वाद का जगत्, फिर रूप का जगत्, फिर शब्द का संसार। एक पर एक नए जगत् उद्घाटित होते गए। अन्धकार से प्रकाश, और भी प्रकाश, और भी और भी ! यहीं तक क्या अन्त है ? कौन बताएगा ? कातर पुकार अब भी जारी है-तमसो मा ज्योतिर्गमय ! न जाने कितने ज्योतिलोक उद्घाटित होनेवाले हैं।
कहते हैं, और ठीक ही कहते होंगे, कि मनुष्य से भिन्न अवर सृष्टि में भी इन्द्रिय गृहीत बिम्ब किसी-न-किसी रूप में रहते हैं पर वहाँ दो बातों की कमी है। इन बिम्बों को विविक्त करने की शक्ति और विविक्तीकृत बिम्बों को अपनी इच्छा से-संकल्पपूर्वक-नये सिरे से नये प्रसार-विस्तार या परम्युटेशन-कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया द्वारा नयी अर्थात् प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओं से भिन्न नयी चीज़ बनाने की क्षमता। शब्द के बिम्बों के विविक्तीकरण का परिणाम भाषा, काव्य और संगीत हैं, रूप-बिम्बों के विविक्तीकरण के फल रंग, उच्चावचता, ह्रस्व-दीर्घ-वर्तुल आदि बिम्ब और फिर संकल्प शक्ति द्वारा विनियुक्त होने पर चित्र, मूर्ति, वास्तु, वस्त्र, अलंकरण, साज-सज्जा आदि। इसी तरह और भी इन्द्रिय गृहीत बिम्बों का विविक्तीकरण, और संकल्प-संयोजन से मानव-सृष्ट सहस्रों नई चीज़ें। यह कोई मामूली बात नहीं है। अभ्यास के कारण इनका महत्त्व भुला दिया जाता है, पर भुलाना चाहिए नहीं। मनुष्य कुछ भुलक्कड़ हो गया है। लेकिन यह बहुत बड़ा दोष भी नहीं है। न भूले तो जीना ही दूभर हो जाए। मगर ऐसी बातों का भूलना ज़रूर बुरा है, जो उसे जीने की शक्ति देती हैं, सीधे खड़ा होने की प्रेरणा देती हैं।
किस दिन एक शुभ मुहूर्त में मनुष्य ने मिट्टी के दिये, रुई की बाती, चकमक की चिनगारी और बीजों से निकलने वाले स्रोत का संयोग देखा। अन्धकार को जीता जा सकता है। दिया जलाया जा सकता है। घने अन्धकार में डूबी धरती को आंशिक रूप में आलोकित किया जा सकता है। अन्धकार से जूझने के संकल्प की जीत हुई। तब से मनुष्य ने इस दिशा में बड़ी प्रगति की है, पर वह आदिम प्रयास क्या भूलने की चीज़ है ? वह मनुष्य की दीर्घकालीन कातर प्रार्थना का उज्ज्वल फल था।
दीवाली याद दिला जाती है उस ज्ञान लोक के अभिनव अंकुर की, जिसने मनुष्य की कातर प्रार्थना को दृढ़ संकल्प का रूप दिया था-अन्धकार से जूझना है, विघ्न-बाधाओं की उपेक्षा करके, संकटों का सामना करके !
इधर कुछ दिनों से शिथिल स्वर सुनाई देने लगे हैं। लोग कहते सुने जाते हैं-अन्धकार महाबलवान् है, उससे जूझने का संकल्प मूढ़ आदर्श मात्र है। सोचता हूँ, यह क्या संकल्प-शक्ति का पराभव है ? क्या मनुष्यता की अवमानना है ? दीवाली आकर कह जाती है, अन्धकार से जूझने का संकल्प ही सही यथार्थ है। मृगमरीचिका में मत भटको। अन्धकार के सैकड़ों परत हैं। उससे जूझना ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। जूझने का संकल्प ही महादेवता है। उसी को प्रत्यक्ष करने की क्रिया को लक्ष्मी की पूजा कहते हैं।
लेकिन मनुष्य के अन्तर्यामी निष्क्रिय नहीं हैं। वे थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते नहीं। वे अधीर भी नहीं होते। वैज्ञानिक का विश्वास है कि अनन्त रुपों में विकसित होते-होते वे मनुष्य के विवेक रूप में प्रत्यक्ष हुए हैं। करोड़ों वर्ष लगे हैं इस रूप में प्रकट होने में। उन्होंने धीरज नहीं छोड़ा। स्पर्शेन्द्रिय से स्वादेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय की और फिर चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रियेन्द्रिय की ओर अपने-आपको अभिव्यक्ति करते हुए मन और बुद्धि के रूप में आविर्भूत हुए हैं। और भी न जाने किन रूपों में अग्रसर हों। वैज्ञानिक को ‘अन्तर्यामी’ शब्द पसन्द नहीं है। कदाचित् वह प्राणशक्ति कहना पसन्द करे। नाम का क्या झगड़ा है ?
जीव का काम पुरा काल में स्पर्श से चल जाता था, बाद में उसने घ्राण शक्ति पाई। वह दूर-दूर की चीज़ों का अन्दाज़ा लगाने लगा। पहले स्पर्श से भिन्न सब कुछ अन्धकार था। अन्तर्यामी रुके नहीं। घ्राण का जगत्, फिर स्वाद का जगत्, फिर रूप का जगत्, फिर शब्द का संसार। एक पर एक नए जगत् उद्घाटित होते गए। अन्धकार से प्रकाश, और भी प्रकाश, और भी और भी ! यहीं तक क्या अन्त है ? कौन बताएगा ? कातर पुकार अब भी जारी है-तमसो मा ज्योतिर्गमय ! न जाने कितने ज्योतिलोक उद्घाटित होनेवाले हैं।
कहते हैं, और ठीक ही कहते होंगे, कि मनुष्य से भिन्न अवर सृष्टि में भी इन्द्रिय गृहीत बिम्ब किसी-न-किसी रूप में रहते हैं पर वहाँ दो बातों की कमी है। इन बिम्बों को विविक्त करने की शक्ति और विविक्तीकृत बिम्बों को अपनी इच्छा से-संकल्पपूर्वक-नये सिरे से नये प्रसार-विस्तार या परम्युटेशन-कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया द्वारा नयी अर्थात् प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओं से भिन्न नयी चीज़ बनाने की क्षमता। शब्द के बिम्बों के विविक्तीकरण का परिणाम भाषा, काव्य और संगीत हैं, रूप-बिम्बों के विविक्तीकरण के फल रंग, उच्चावचता, ह्रस्व-दीर्घ-वर्तुल आदि बिम्ब और फिर संकल्प शक्ति द्वारा विनियुक्त होने पर चित्र, मूर्ति, वास्तु, वस्त्र, अलंकरण, साज-सज्जा आदि। इसी तरह और भी इन्द्रिय गृहीत बिम्बों का विविक्तीकरण, और संकल्प-संयोजन से मानव-सृष्ट सहस्रों नई चीज़ें। यह कोई मामूली बात नहीं है। अभ्यास के कारण इनका महत्त्व भुला दिया जाता है, पर भुलाना चाहिए नहीं। मनुष्य कुछ भुलक्कड़ हो गया है। लेकिन यह बहुत बड़ा दोष भी नहीं है। न भूले तो जीना ही दूभर हो जाए। मगर ऐसी बातों का भूलना ज़रूर बुरा है, जो उसे जीने की शक्ति देती हैं, सीधे खड़ा होने की प्रेरणा देती हैं।
किस दिन एक शुभ मुहूर्त में मनुष्य ने मिट्टी के दिये, रुई की बाती, चकमक की चिनगारी और बीजों से निकलने वाले स्रोत का संयोग देखा। अन्धकार को जीता जा सकता है। दिया जलाया जा सकता है। घने अन्धकार में डूबी धरती को आंशिक रूप में आलोकित किया जा सकता है। अन्धकार से जूझने के संकल्प की जीत हुई। तब से मनुष्य ने इस दिशा में बड़ी प्रगति की है, पर वह आदिम प्रयास क्या भूलने की चीज़ है ? वह मनुष्य की दीर्घकालीन कातर प्रार्थना का उज्ज्वल फल था।
दीवाली याद दिला जाती है उस ज्ञान लोक के अभिनव अंकुर की, जिसने मनुष्य की कातर प्रार्थना को दृढ़ संकल्प का रूप दिया था-अन्धकार से जूझना है, विघ्न-बाधाओं की उपेक्षा करके, संकटों का सामना करके !
इधर कुछ दिनों से शिथिल स्वर सुनाई देने लगे हैं। लोग कहते सुने जाते हैं-अन्धकार महाबलवान् है, उससे जूझने का संकल्प मूढ़ आदर्श मात्र है। सोचता हूँ, यह क्या संकल्प-शक्ति का पराभव है ? क्या मनुष्यता की अवमानना है ? दीवाली आकर कह जाती है, अन्धकार से जूझने का संकल्प ही सही यथार्थ है। मृगमरीचिका में मत भटको। अन्धकार के सैकड़ों परत हैं। उससे जूझना ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। जूझने का संकल्प ही महादेवता है। उसी को प्रत्यक्ष करने की क्रिया को लक्ष्मी की पूजा कहते हैं।
आलोक-पर्व की ज्योतिर्मय देवी
मार्कण्डेय पुराण के अनुसार समस्त सृष्टि की मूलभूत आद्याशक्ति महालक्ष्मी है। वह सत्व, सज और तम तीनों गुणों का मूल समवाय है। वही आद्याशक्ति है। वह समस्त विश्व में व्याप्त होकर विराजमान है। वह लक्ष्य और अलक्ष्य, इन दो रूपों में रहती है। लक्ष्य रूप में यह चराचर जगत ही उसका स्वरूप है और-अलक्ष्य रूप में यह समस्त जगत् की सृष्टि का मूल कारण है। उसी से विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। दीपावली को इसी महालक्ष्मी का पूजन होता है। तामसिक रूप में वह क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, कालरात्रि, महामारी के रूप में अभिव्यक्ति होती है, राजसिक रूप में वह जगत् का भरण-पोषण करने वाली ‘श्री’ के रूप में उन लोगों के घर में आती है, जिन्होंने पूर्व-जन्म में शुभ कर्म किए होते हैं; परन्तु यदि इस जन्म में उनकी वृत्तिपाप की ओर जाती है, तो वह भयंकर अलक्ष्मी बन जाती है। सात्त्विक रूप में वह महाविद्या, महावाणी भारती वाक् सरस्वती के रूप में अभिव्यक्त होती है। मूल आद्याशक्ति ही महालक्ष्मी है।
शास्त्रों में भी ऐसे वचन मिल जाते हैं, जिनमें महाकाली या महासरस्वती को ही आद्याशक्ति कहा गया है। जो लोग हिन्दू शास्त्रों की पद्धति से परिचित नहीं होते, वे साधारणतः इस प्रकार की बातों को देखकर कह उठते हैं कि यह ‘बहुदेववाद’ है। यूरोपियन पंडितों ने इसके लिए ‘पालिथीज़्म’ शब्द का प्रयोग किया है। पालिथीज़्म या बहुदेववाद से एक ऐसे धर्म का बोध होता है, जिसमें अनेक छोटे-देवताओं की मण्डली में विश्वास किया जाता है। इन देवताओं की मर्यादा और अधिकार निश्चित होते हैं। जो लोग हिन्दू शास्त्रों की थोड़ी भी गहराई में जाना आवश्यक समझते हैं, वे इस बात को कभी नहीं स्वीकार कर सकते। मैक्समूलर ने बहुत पहले बताया था कि वेदों में पाया जानेवाला ‘बहुदेववाद’ वस्तुतः बहुदेववाद है है ही नहीं; क्योंकि न तो वह ग्रीक-रोमन बहुदेववाद के समान है, जिसमें बहुत-से देव-देवी एक महादेवता के अधीन होते हैं और न अफ्रीका आदि देशों की आदिम जातियों में पाए जानेवाले बहुदेववाद के समान है जिसमें छोटे-मोटे अनेक देवता स्वतन्त्र होते हैं। मैक्समूलर ने इस विश्वास के लिए एक शब्द सुझाया था-हेनोथीज्म, जिसे हिन्दी में ‘एकैकदेववाद’ शब्द से कुछ-कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के धार्मिक विश्वास में अनेक देवता की उपासना होती अवश्य है, पर जिस देवता की उपासना चलती रहती है, उसे ही सारे देवताओं से श्रेष्ठ और सबका हेतुभूत माना जाता है। जैसे जब इन्द्र की उपासना का प्रसंग होगा, तो कहा जाएगा कि इन्द्र ही आदि देव हैं, वरुण, यम, सूर्य, चन्द्र, अग्नि सबका वह स्वामी है और सबका मूलभूत है। पर जब अग्नि की उपासना का प्रसंग होगा तो कहा जायेगा कि अग्नि ही मुख्य देवता है और इन्द्र, वरुण आदि का स्वामी है और सबका मूलभूत देवता है, इत्यादि।
परन्तु थोड़ी और गहराई में जाकर देखा जाये तो इसका स्पष्ट रूप अद्वैतवाद है। एक ही देवता है, जो विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। उपासना के समय उसके जिस विशिष्ट रूप का ध्यान किया जाता है, वही समस्त अन्य रूपों में मुख्य और आदिभूत माना जाता है। इसका रहस्य यह है कि साधक सदा मूल अद्वैत सत्ता के प्रति सजग रहता है। अपनी रुचि और संस्कारों और कभी-कभी प्रयोजन के अनुसार वह उपास्य के विशिष्ट रूप की उपासना अवश्य करता है, परन्तु शास्त्र उसे कभी भूलने नहीं देना चाहता कि रूप कोई हो, है वह मूल अद्वैत सत्ता की ही अभिव्यक्ति। इस प्रकार हिन्दू शास्त्रों की इस पद्धति का रहस्य यही है कि उपास्य वस्तुतः मूल अद्वैत सत्ता का ही रूप है। इसी बात को और भी स्पष्ट करके वैदिक ऋषि ने कहा था कि जो देवता अग्नि में है, जल में है, वायु में है, औषधियों में है, वनस्पतियों में है, उसी महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ !
आज से कोई दो हज़ार वर्ष पहले से इस देश के धार्मिक साहित्य में और शिल्प और कला में यह विश्वास मुखर हो उठा है कि उपास्य वस्तुतः देवता की शक्ति होती है। यह नहीं है कि यह विचार नया है, पहले था ही नहीं, पर उपलब्ध धार्मिक साहित्य और शिल्प और कला-सामग्री में यह बात इस समय से अधिक व्यापक रूप में और अत्यधिक मुखर भाव से प्रकट हुई दिखती है। इस विश्वास का सबसे बड़ा आवश्यक अंग यह है कि शक्ति और शक्तिमान् में कोई तात्विक भेद नहीं है, दोनों एक हैं ! चन्द्रमा और चन्द्रिका की भाँति वे अलग-अलग प्रतीत होकर भी तत्त्वतः एक हैं-अन्तर नैव जानीमश्चन्द्र-चन्द्रिकयोरिव। परन्तु उपास्य शक्ति ही है। जो लोग इस विश्वास को अपनी तर्कसम्मत सीमा तक खींचकर ले जाते हैं, वे शक्त कहलाते हैं। जो शक्ति और शक्तिमान् के एकत्व पर अधिक ज़ोर देते हैं, वे शाक्त नहीं कहलाते। मगर कहलाते हों या न कहलाते हों, शक्ति की उपास्यता पर विश्वास दोनों का है। जिन लोगों ने संसार की भरण-पोषण करनेवाली वैष्णवी शक्ति को मुख्य रूप से उपास्य माना है, उन्होंने उस आदिभूता शक्ति का नाम ‘महालक्ष्मी’ स्वीकार किया है। दीपावली के पुण्य-पर्व पर इसी आद्याशक्ति की पूजा होती है। देश के पूर्वी हिस्सों में इस दिन महाकाली की पूजा होती है। दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। केवल रुचि और संस्कार के अनुसार आद्याशक्ति के विशिष्ट रूपों पर बल दिया जाता है। पूजा आद्याशक्ति की ही होती है। मुझे यह ठीक-ठीक नहीं मालूम कि देश के किसी कोने में इस दिन महासरस्वती की पूजा होती है या नहीं। होती हो तो कुछ अचरज की बात नहीं होगी। दीपावली का पर्व आद्याशक्ति के विभिन्न रूपों के स्मरण का दिन है।
यह सारा दृश्यमान जगत् ज्ञान, इच्छा और क्रिया के रूप में त्रिटुपीकृत है। ब्रह्म की मूल शक्ति में इन तीनों का सूक्ष्म रूप में अवस्थान होगा। त्रिपुटीकृत जगत की मूल कारणभूता इस शक्ति को ‘त्रिपुरा’ भी कहा जाता है। आरम्भ में जिसे महालक्ष्मी कहा गया है उससे यह अभिन्न है। ज्ञान रूप में अभिव्यक्त होने पर सत्त्वगुणप्रधान सरस्वती के रूप में, इच्छा रूप में रजोगुण प्रधान लक्ष्मी के रुप में और क्रिया रुप में तमोगुण-प्रधान काली के रुप में उपास्य होती है। लक्ष्मी इच्छा रुप में अभिव्यक्त होती है। जो साधक लक्ष्मी रूप में आद्याशक्ति की उपासना करते हैं, उनके चित्त में इच्छा तत्त्व की प्रधानता होती है, पर बाकी दो तत्त्व-ज्ञान और क्रिया-भी उसमें सहायक होते हैं। इसीलिए लक्ष्मी की उपासना ‘ज्ञानपूर्वा क्रियापरा’ होती है, अर्थात् वह ज्ञान द्वारा चालित और क्रिया द्वारा अनुगमित इच्छा-शक्ति की उपासना होती है। ‘ज्ञानपूर्वा क्रियापरा’ का मतलब है कि यद्यपि इच्छा-शक्ति ही मुख्यतया उपास्य है, पर पहले ज्ञान की सहायता और बाद में क्रिया का समर्थन इसमें आवश्यक है। यदि उल्टा हो जाये, अर्थात् इच्छा शक्ति की उपासना क्रियापूर्वा और ज्ञानपरा हो जाये, तो उपासना का रूप बदल जाता है। पहली अवस्था में उपास्या लक्ष्मी समस्त जगत् के उपकार के लिए होती है। उस लक्ष्मी का वाहन गरुड़ होता है। गरुड़ शक्ति, वेग और सेवावृत्ति का प्रतीक है। दूसरी अवस्था में उसका वाहन उल्लू होता है। उल्लू स्वार्थ, अन्धकारप्रियता और विच्छिन्नता का प्रतीक है। लक्ष्मी तभी उपास्य होकर भक्त को ठीक-ठीक कृतकृत्य करती है। तब उसके चित्त में सबके कल्याण की कामना रहती है। यदि केवल अपना स्वार्थ ही साधक के चित्त में प्रधान हो, तो वह उलूकवाहिनी शक्ति की ही कृपा पा सकता है। फिर तो वह तमोगुण का शिकार हो जाता है। उसकी उपासना लोकल्याण-मार्ग से विच्छिन्न होकर बन्ध्या हो जाती है। दीपावली प्रकाश का पर्व है। इस दिन जिस लक्ष्मी की पूजा होती है, वह गरुड़वाहिनी है-शक्ति, सेवा और गतिशीलता उसके मुख्य गुण हैं। प्रकाश और अन्धकार का नियत विरोध है। अमावस्या की रात को प्रयत्नपूर्वक लाख-लाख प्रदीपों को जलाकर हम लक्ष्मी के उलूकवाहिनी रूप की नहीं, गरुड़वाहिनी रूप की उपासना करते हैं। हम अन्धकार का, समाज से कटकर रहने का, स्वार्थपरता का प्रयत्नपूर्वक प्रत्याख्यान करते हैं और प्रकाश का, सामाजिकता का और सेवावृत्ति का आह्वान करते हैं। हमें भूलना न चाहिए कि यह उपासना ज्ञान द्वारा चालित और क्रिया द्वारा अनुगमित होकर ही सार्थक होती है-
शास्त्रों में भी ऐसे वचन मिल जाते हैं, जिनमें महाकाली या महासरस्वती को ही आद्याशक्ति कहा गया है। जो लोग हिन्दू शास्त्रों की पद्धति से परिचित नहीं होते, वे साधारणतः इस प्रकार की बातों को देखकर कह उठते हैं कि यह ‘बहुदेववाद’ है। यूरोपियन पंडितों ने इसके लिए ‘पालिथीज़्म’ शब्द का प्रयोग किया है। पालिथीज़्म या बहुदेववाद से एक ऐसे धर्म का बोध होता है, जिसमें अनेक छोटे-देवताओं की मण्डली में विश्वास किया जाता है। इन देवताओं की मर्यादा और अधिकार निश्चित होते हैं। जो लोग हिन्दू शास्त्रों की थोड़ी भी गहराई में जाना आवश्यक समझते हैं, वे इस बात को कभी नहीं स्वीकार कर सकते। मैक्समूलर ने बहुत पहले बताया था कि वेदों में पाया जानेवाला ‘बहुदेववाद’ वस्तुतः बहुदेववाद है है ही नहीं; क्योंकि न तो वह ग्रीक-रोमन बहुदेववाद के समान है, जिसमें बहुत-से देव-देवी एक महादेवता के अधीन होते हैं और न अफ्रीका आदि देशों की आदिम जातियों में पाए जानेवाले बहुदेववाद के समान है जिसमें छोटे-मोटे अनेक देवता स्वतन्त्र होते हैं। मैक्समूलर ने इस विश्वास के लिए एक शब्द सुझाया था-हेनोथीज्म, जिसे हिन्दी में ‘एकैकदेववाद’ शब्द से कुछ-कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के धार्मिक विश्वास में अनेक देवता की उपासना होती अवश्य है, पर जिस देवता की उपासना चलती रहती है, उसे ही सारे देवताओं से श्रेष्ठ और सबका हेतुभूत माना जाता है। जैसे जब इन्द्र की उपासना का प्रसंग होगा, तो कहा जाएगा कि इन्द्र ही आदि देव हैं, वरुण, यम, सूर्य, चन्द्र, अग्नि सबका वह स्वामी है और सबका मूलभूत है। पर जब अग्नि की उपासना का प्रसंग होगा तो कहा जायेगा कि अग्नि ही मुख्य देवता है और इन्द्र, वरुण आदि का स्वामी है और सबका मूलभूत देवता है, इत्यादि।
परन्तु थोड़ी और गहराई में जाकर देखा जाये तो इसका स्पष्ट रूप अद्वैतवाद है। एक ही देवता है, जो विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। उपासना के समय उसके जिस विशिष्ट रूप का ध्यान किया जाता है, वही समस्त अन्य रूपों में मुख्य और आदिभूत माना जाता है। इसका रहस्य यह है कि साधक सदा मूल अद्वैत सत्ता के प्रति सजग रहता है। अपनी रुचि और संस्कारों और कभी-कभी प्रयोजन के अनुसार वह उपास्य के विशिष्ट रूप की उपासना अवश्य करता है, परन्तु शास्त्र उसे कभी भूलने नहीं देना चाहता कि रूप कोई हो, है वह मूल अद्वैत सत्ता की ही अभिव्यक्ति। इस प्रकार हिन्दू शास्त्रों की इस पद्धति का रहस्य यही है कि उपास्य वस्तुतः मूल अद्वैत सत्ता का ही रूप है। इसी बात को और भी स्पष्ट करके वैदिक ऋषि ने कहा था कि जो देवता अग्नि में है, जल में है, वायु में है, औषधियों में है, वनस्पतियों में है, उसी महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ !
आज से कोई दो हज़ार वर्ष पहले से इस देश के धार्मिक साहित्य में और शिल्प और कला में यह विश्वास मुखर हो उठा है कि उपास्य वस्तुतः देवता की शक्ति होती है। यह नहीं है कि यह विचार नया है, पहले था ही नहीं, पर उपलब्ध धार्मिक साहित्य और शिल्प और कला-सामग्री में यह बात इस समय से अधिक व्यापक रूप में और अत्यधिक मुखर भाव से प्रकट हुई दिखती है। इस विश्वास का सबसे बड़ा आवश्यक अंग यह है कि शक्ति और शक्तिमान् में कोई तात्विक भेद नहीं है, दोनों एक हैं ! चन्द्रमा और चन्द्रिका की भाँति वे अलग-अलग प्रतीत होकर भी तत्त्वतः एक हैं-अन्तर नैव जानीमश्चन्द्र-चन्द्रिकयोरिव। परन्तु उपास्य शक्ति ही है। जो लोग इस विश्वास को अपनी तर्कसम्मत सीमा तक खींचकर ले जाते हैं, वे शक्त कहलाते हैं। जो शक्ति और शक्तिमान् के एकत्व पर अधिक ज़ोर देते हैं, वे शाक्त नहीं कहलाते। मगर कहलाते हों या न कहलाते हों, शक्ति की उपास्यता पर विश्वास दोनों का है। जिन लोगों ने संसार की भरण-पोषण करनेवाली वैष्णवी शक्ति को मुख्य रूप से उपास्य माना है, उन्होंने उस आदिभूता शक्ति का नाम ‘महालक्ष्मी’ स्वीकार किया है। दीपावली के पुण्य-पर्व पर इसी आद्याशक्ति की पूजा होती है। देश के पूर्वी हिस्सों में इस दिन महाकाली की पूजा होती है। दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। केवल रुचि और संस्कार के अनुसार आद्याशक्ति के विशिष्ट रूपों पर बल दिया जाता है। पूजा आद्याशक्ति की ही होती है। मुझे यह ठीक-ठीक नहीं मालूम कि देश के किसी कोने में इस दिन महासरस्वती की पूजा होती है या नहीं। होती हो तो कुछ अचरज की बात नहीं होगी। दीपावली का पर्व आद्याशक्ति के विभिन्न रूपों के स्मरण का दिन है।
यह सारा दृश्यमान जगत् ज्ञान, इच्छा और क्रिया के रूप में त्रिटुपीकृत है। ब्रह्म की मूल शक्ति में इन तीनों का सूक्ष्म रूप में अवस्थान होगा। त्रिपुटीकृत जगत की मूल कारणभूता इस शक्ति को ‘त्रिपुरा’ भी कहा जाता है। आरम्भ में जिसे महालक्ष्मी कहा गया है उससे यह अभिन्न है। ज्ञान रूप में अभिव्यक्त होने पर सत्त्वगुणप्रधान सरस्वती के रूप में, इच्छा रूप में रजोगुण प्रधान लक्ष्मी के रुप में और क्रिया रुप में तमोगुण-प्रधान काली के रुप में उपास्य होती है। लक्ष्मी इच्छा रुप में अभिव्यक्त होती है। जो साधक लक्ष्मी रूप में आद्याशक्ति की उपासना करते हैं, उनके चित्त में इच्छा तत्त्व की प्रधानता होती है, पर बाकी दो तत्त्व-ज्ञान और क्रिया-भी उसमें सहायक होते हैं। इसीलिए लक्ष्मी की उपासना ‘ज्ञानपूर्वा क्रियापरा’ होती है, अर्थात् वह ज्ञान द्वारा चालित और क्रिया द्वारा अनुगमित इच्छा-शक्ति की उपासना होती है। ‘ज्ञानपूर्वा क्रियापरा’ का मतलब है कि यद्यपि इच्छा-शक्ति ही मुख्यतया उपास्य है, पर पहले ज्ञान की सहायता और बाद में क्रिया का समर्थन इसमें आवश्यक है। यदि उल्टा हो जाये, अर्थात् इच्छा शक्ति की उपासना क्रियापूर्वा और ज्ञानपरा हो जाये, तो उपासना का रूप बदल जाता है। पहली अवस्था में उपास्या लक्ष्मी समस्त जगत् के उपकार के लिए होती है। उस लक्ष्मी का वाहन गरुड़ होता है। गरुड़ शक्ति, वेग और सेवावृत्ति का प्रतीक है। दूसरी अवस्था में उसका वाहन उल्लू होता है। उल्लू स्वार्थ, अन्धकारप्रियता और विच्छिन्नता का प्रतीक है। लक्ष्मी तभी उपास्य होकर भक्त को ठीक-ठीक कृतकृत्य करती है। तब उसके चित्त में सबके कल्याण की कामना रहती है। यदि केवल अपना स्वार्थ ही साधक के चित्त में प्रधान हो, तो वह उलूकवाहिनी शक्ति की ही कृपा पा सकता है। फिर तो वह तमोगुण का शिकार हो जाता है। उसकी उपासना लोकल्याण-मार्ग से विच्छिन्न होकर बन्ध्या हो जाती है। दीपावली प्रकाश का पर्व है। इस दिन जिस लक्ष्मी की पूजा होती है, वह गरुड़वाहिनी है-शक्ति, सेवा और गतिशीलता उसके मुख्य गुण हैं। प्रकाश और अन्धकार का नियत विरोध है। अमावस्या की रात को प्रयत्नपूर्वक लाख-लाख प्रदीपों को जलाकर हम लक्ष्मी के उलूकवाहिनी रूप की नहीं, गरुड़वाहिनी रूप की उपासना करते हैं। हम अन्धकार का, समाज से कटकर रहने का, स्वार्थपरता का प्रयत्नपूर्वक प्रत्याख्यान करते हैं और प्रकाश का, सामाजिकता का और सेवावृत्ति का आह्वान करते हैं। हमें भूलना न चाहिए कि यह उपासना ज्ञान द्वारा चालित और क्रिया द्वारा अनुगमित होकर ही सार्थक होती है-
सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुण परमेश्वरी।
लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता।।
लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता।।
प्राचीन भारत में मदनोत्सव
संस्कृत के किसी भी काव्य, नाटक, कथा और आख्यायिका को पढ़िए वसन्त ऋतु का उत्सव उसमें किसी-न-किसी बहाने अवश्य आ जायेगा। कालिदास तो वसन्तोत्सव का बहाना ढूँढ़ते रहते-से लगते हैं। मेघदूत वर्षा ऋतु का काव्य है, पर यक्षप्रिया के उद्यान के वर्णन के प्रसंग में प्रिया के नूपुरयुक्त वामचरणों के मृदुल आघात से कंधे पर से फूट-उठनेवाले अशोक और मुख-मदिरा से सिंचकर खिल उठने को लालायित वकुल की चर्चा उसमें आ ही गई है। वस्तुतः अशोक और वकुल को इस प्रकार खिला देने का उत्सव वसंत में ही मनाया जाता था। वसन्त का समय प्राचीन भारत में उत्सवों का काल हुआ करता था। कामसूत्र में इस समय के कई-उत्सवों की चर्चा आती है। इनमें दो बहुत प्रसिद्ध हैं-मदनोत्सव और सुवसन्तक। कामसूत्र के टीकाकार यशोधर ने दोनों को एक मान लिया है, पर अन्य ग्रंथों से स्पष्ट है कि ये दोनों उत्सव अलग-अलग दिनों को मनाए जाते थे। भोजदेव के अनुसार सुवसंतक वसंतावतार का उत्सव है-आजकल का वसन्तपंचमी का उत्सव। मदनोत्सव होली के रूप में आज भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। वात्स्यायन के कामसूत्र में भी इसका उल्लेख है।
पुराने ग्रन्थों से पता चलता है कि फागुन से आरंभ करके चैत के महीने तक वसन्तोत्सव कई प्रकार से मनाया जाता था। उसके दो रूप बहुत प्रसिद्ध थे। एक सार्वजनिक धूम-धाम का और दूसरा कामदेव के पूजन का। सम्राट हर्षदेव की रत्नावली नाटिका में इन दोनों प्रकार के उत्सवों का बड़ा ही सरस और जीवन्त वर्णन मिलता है। उस दिन सारा नगर पुरवासियों की करतल ध्वनि, मधुर संगीत और मृदंग के मादक घोष से मुखरित हो उठता था। नागर जन मदमत्त हो उठते थे। राजा अपने ऊँचे प्रासाद की सबसे ऊँची चन्द्रशाला में बैठकर नगरवासियों के आमोद-प्रमोद का रस लेते थे। नागरिकाएँ मधुमास से मत्त होकर सामने पड़ जानेवाले किसी भी पुरुष को पिचकारी (श्रृंगक) के रंगीन जल से सराबोर कर देती थीं। राज-मार्गों के चौराहों पर मर्दल नाम के ढोल और चर्चरी गीत की ध्वनियाँ मुखरित हो उठती थीं। सुंगधित पिष्टातक (अबीर) से दिशाएँ रंगीन हो उठती थीं। केशर मिश्रित पिष्टातक से राजपथ और प्रासाद इस प्रकार आच्छादित हो उठते थे कि प्रातःकालीन उषा की छाया का भ्रम होने लगता था। नगरजनों के शरीर पर शोभमान हेमालंकार और सिर पर धारण किए हुए अशोक के लाल-लाल फूल इस सुनहरी आभा को और भी बढ़ा देते थे। ऐसा जान पड़ता था कि कुबेर को भी अपनी समृद्धि से जीतने का दावा करनेवाली सारी नगरी सुनहरे रंग में डुबो दी गयी है-
पुराने ग्रन्थों से पता चलता है कि फागुन से आरंभ करके चैत के महीने तक वसन्तोत्सव कई प्रकार से मनाया जाता था। उसके दो रूप बहुत प्रसिद्ध थे। एक सार्वजनिक धूम-धाम का और दूसरा कामदेव के पूजन का। सम्राट हर्षदेव की रत्नावली नाटिका में इन दोनों प्रकार के उत्सवों का बड़ा ही सरस और जीवन्त वर्णन मिलता है। उस दिन सारा नगर पुरवासियों की करतल ध्वनि, मधुर संगीत और मृदंग के मादक घोष से मुखरित हो उठता था। नागर जन मदमत्त हो उठते थे। राजा अपने ऊँचे प्रासाद की सबसे ऊँची चन्द्रशाला में बैठकर नगरवासियों के आमोद-प्रमोद का रस लेते थे। नागरिकाएँ मधुमास से मत्त होकर सामने पड़ जानेवाले किसी भी पुरुष को पिचकारी (श्रृंगक) के रंगीन जल से सराबोर कर देती थीं। राज-मार्गों के चौराहों पर मर्दल नाम के ढोल और चर्चरी गीत की ध्वनियाँ मुखरित हो उठती थीं। सुंगधित पिष्टातक (अबीर) से दिशाएँ रंगीन हो उठती थीं। केशर मिश्रित पिष्टातक से राजपथ और प्रासाद इस प्रकार आच्छादित हो उठते थे कि प्रातःकालीन उषा की छाया का भ्रम होने लगता था। नगरजनों के शरीर पर शोभमान हेमालंकार और सिर पर धारण किए हुए अशोक के लाल-लाल फूल इस सुनहरी आभा को और भी बढ़ा देते थे। ऐसा जान पड़ता था कि कुबेर को भी अपनी समृद्धि से जीतने का दावा करनेवाली सारी नगरी सुनहरे रंग में डुबो दी गयी है-
कीर्णौ:पिष्टातकौघैः कृतदिवसमुखैः कुंकुमस्नातगौरैः
हेमालंकारभाभिर्भरनमितशिखैः शेखरैः कैंकिरातैः।
एषा वेषाभिलक्ष्यस्वभवनविजिताशेषवित्तेकोशा
कौशाम्बी शातकुभ्भद्रवखचितजनेवैकपीता विभाति।
हेमालंकारभाभिर्भरनमितशिखैः शेखरैः कैंकिरातैः।
एषा वेषाभिलक्ष्यस्वभवनविजिताशेषवित्तेकोशा
कौशाम्बी शातकुभ्भद्रवखचितजनेवैकपीता विभाति।
रत्नावलि-1.11
उस दिन बड़े घरों के सामने आँगन फव्वारे पूरे वेग से छूटते रहते थे और नागरिकाओं की, अपनी पिचकारी में पानी भरने की उल्लास-लालसा को पूरा करने में सहायक हुआ करते थे। इस स्थान पर पौर-युवतियों के बराबर आते रहने से उनके सीमन्त के सिंदूर और कपोलों के अबीर भरते रहते थे और सारा फर्श लाल-कीचड़ से भर जाता था, फर्श सिंदूरमय हो उठता था-
धारायंत्रविमुक्तसंततपयः पूरप्लुते सर्वतः
सद्यःसान्द्रविमर्दकर्दमकृतकीडे क्षणं प्रांगणे।
उद्दामप्रमदाकपोलनिपततसिन्दूररागारुणैः
सैन्दूरीक्रियते जनेन चरणन्यासैः पुरः कुट्टिमम्।।
सद्यःसान्द्रविमर्दकर्दमकृतकीडे क्षणं प्रांगणे।
उद्दामप्रमदाकपोलनिपततसिन्दूररागारुणैः
सैन्दूरीक्रियते जनेन चरणन्यासैः पुरः कुट्टिमम्।।
मगर इस उत्सव का सर्वाधिक हुड़दंगी रूप वार-वनिताओं के मुहल्ले के वर्णन में मिलता है। निस्संदेह यह होली का पुराना रूप है।
इसके साथ ही इस उत्सव का एक शान्त स्निग्ध चित्र भी मिलता है। भवभूति के मालती-माधव नामक प्रकरण में एक मदनोत्सव का चित्र है। इससे पता चलता है कि मदनोद्यान-जो विशेष रूप से इस उत्सव के लिए ही बनाया जाता था- इसका मुख्य केन्द्र हुआ करता था। इसमें कामदेव का मंदिर हुआ करता था। इसी उद्यान में नगर के स्त्री-पुरुष एकत्र होकर भगवान कन्दर्प की पूजा करते थे। यहाँ पर लोग अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार फूल चुनते, माला बनाते, अबीर-कुंकुम से क्रीड़ा करते और नृत्य-गीत आदि से मनोविनोद किया करते थे। इस मंदिर में प्रतिष्ठित परिवारों की कन्याएँ भी पूजनार्थ आया करती थीं और मदन देवता की पूजा करके मनोवांछित वर की प्रार्थना करती थीं। जनता की भीड़ प्रातःकाल से ही शुरू हो जाती थी और संध्याकाल तक अबाध गति से आती रहती थी। मालती-माधव से पता चलता है कि अमात्य भूरिवसु की कन्या मालती भी इस उद्यान में कन्दर्प-पूजन के लिए आई थी। इस पूजन में धार्मिक बुद्धि की प्रधानता होती थी और शोरगुल और हुड़दंग का नाम भी नहीं था। यह मंदिर नगर के बाहर हुआ करता था।
मदन देवता की एक पूजा चैत्र के महीने में होती थी। अशोक वृक्ष के नीचे मिट्टी का कलश-स्थापित किया जाता था। सफेद चावल भरे जाते थे। फलों और ईख का रस इस पूजा में नैवेद्य थे। कलश को सफेद वस्त्र से ढका जाता था। चन्दन भी उस पर सफेद ही छिड़का जाता था। कलश के ऊपर ताम्र पत्र पर केले के पत्ते रखे जाते थे, जिस पर कामदेव और रति की प्रतिमा उतारी जाती थी और नाना भाँति के गंध, धूप, नृत्य, गीत आदि से देवताओं को तृप्त किया जाता था। यह मतस्यपुराण की बात है। इसके दूसरे दिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भी पूजा होती थी। लोग व्रत रखते थे।
शिल्परत्न, विष्णुधर्मोत्तर पुराण आदि ग्रन्थों में कामदेव की प्रतिमा बनाने की विधियाँ दी गई है। विष्णुधर्मोत्तर के अनुसार उसके आठ भुज हैं, चार पत्नियाँ; परन्तु शिल्परत्न में केवल यही कहा गया है कि वह अपूर्व सुन्दर हो और उसकी बायीं ओर अभिलाषवती रति और दाहिनी ओर गृहकर्म-निरता प्रीति ये दो पत्नियाँ हों। स्थायी मंदिरों में दोनों प्रकार की मूर्तियाँ बनती थीं, पर अशोक वृक्ष के नीचे जो मूर्ति बनती थी वह द्विभुज ही होती होगी। रत्नावली नाटक में राजा को अशोक वृक्ष के नीचे बैठा देखकर रत्नावली को भ्रम हो गया था कि कामदेव साक्षात् आकर पूजा ग्रहण करते हैं।
कालिदास के मालविकाग्निमित्र और श्री हर्षदेव की रत्नावली में इस उत्सव के सर्वाधिक सरस अनुष्ठान, अशोक में पुष्प ले आने का विवरण मिल जाता है। भोजराज और श्री हर्षदेव की गवाही पर कहा जा सकता है उस दिन सुन्दरियाँ कुसुंभी भी रंग की साड़ी पहनती थीं। तुरन्त स्नान करने से रानी वासवदत्ता की शरीर-कान्ति और भी निखर आई थी, वह कौसुंभ राग से रंजित साड़ी पहनकर जब अशोक वृक्ष के नीचे कामदेव की पूजा कर रही थी तो उसकी साड़ी का लाल पल्ला फड़फड़ा उठा था। उस समय राजा को ऐसा लगा था, जैसे तरुण प्रवाल विटप की लता ही लहरा उठी हो-
इसके साथ ही इस उत्सव का एक शान्त स्निग्ध चित्र भी मिलता है। भवभूति के मालती-माधव नामक प्रकरण में एक मदनोत्सव का चित्र है। इससे पता चलता है कि मदनोद्यान-जो विशेष रूप से इस उत्सव के लिए ही बनाया जाता था- इसका मुख्य केन्द्र हुआ करता था। इसमें कामदेव का मंदिर हुआ करता था। इसी उद्यान में नगर के स्त्री-पुरुष एकत्र होकर भगवान कन्दर्प की पूजा करते थे। यहाँ पर लोग अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार फूल चुनते, माला बनाते, अबीर-कुंकुम से क्रीड़ा करते और नृत्य-गीत आदि से मनोविनोद किया करते थे। इस मंदिर में प्रतिष्ठित परिवारों की कन्याएँ भी पूजनार्थ आया करती थीं और मदन देवता की पूजा करके मनोवांछित वर की प्रार्थना करती थीं। जनता की भीड़ प्रातःकाल से ही शुरू हो जाती थी और संध्याकाल तक अबाध गति से आती रहती थी। मालती-माधव से पता चलता है कि अमात्य भूरिवसु की कन्या मालती भी इस उद्यान में कन्दर्प-पूजन के लिए आई थी। इस पूजन में धार्मिक बुद्धि की प्रधानता होती थी और शोरगुल और हुड़दंग का नाम भी नहीं था। यह मंदिर नगर के बाहर हुआ करता था।
मदन देवता की एक पूजा चैत्र के महीने में होती थी। अशोक वृक्ष के नीचे मिट्टी का कलश-स्थापित किया जाता था। सफेद चावल भरे जाते थे। फलों और ईख का रस इस पूजा में नैवेद्य थे। कलश को सफेद वस्त्र से ढका जाता था। चन्दन भी उस पर सफेद ही छिड़का जाता था। कलश के ऊपर ताम्र पत्र पर केले के पत्ते रखे जाते थे, जिस पर कामदेव और रति की प्रतिमा उतारी जाती थी और नाना भाँति के गंध, धूप, नृत्य, गीत आदि से देवताओं को तृप्त किया जाता था। यह मतस्यपुराण की बात है। इसके दूसरे दिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भी पूजा होती थी। लोग व्रत रखते थे।
शिल्परत्न, विष्णुधर्मोत्तर पुराण आदि ग्रन्थों में कामदेव की प्रतिमा बनाने की विधियाँ दी गई है। विष्णुधर्मोत्तर के अनुसार उसके आठ भुज हैं, चार पत्नियाँ; परन्तु शिल्परत्न में केवल यही कहा गया है कि वह अपूर्व सुन्दर हो और उसकी बायीं ओर अभिलाषवती रति और दाहिनी ओर गृहकर्म-निरता प्रीति ये दो पत्नियाँ हों। स्थायी मंदिरों में दोनों प्रकार की मूर्तियाँ बनती थीं, पर अशोक वृक्ष के नीचे जो मूर्ति बनती थी वह द्विभुज ही होती होगी। रत्नावली नाटक में राजा को अशोक वृक्ष के नीचे बैठा देखकर रत्नावली को भ्रम हो गया था कि कामदेव साक्षात् आकर पूजा ग्रहण करते हैं।
कालिदास के मालविकाग्निमित्र और श्री हर्षदेव की रत्नावली में इस उत्सव के सर्वाधिक सरस अनुष्ठान, अशोक में पुष्प ले आने का विवरण मिल जाता है। भोजराज और श्री हर्षदेव की गवाही पर कहा जा सकता है उस दिन सुन्दरियाँ कुसुंभी भी रंग की साड़ी पहनती थीं। तुरन्त स्नान करने से रानी वासवदत्ता की शरीर-कान्ति और भी निखर आई थी, वह कौसुंभ राग से रंजित साड़ी पहनकर जब अशोक वृक्ष के नीचे कामदेव की पूजा कर रही थी तो उसकी साड़ी का लाल पल्ला फड़फड़ा उठा था। उस समय राजा को ऐसा लगा था, जैसे तरुण प्रवाल विटप की लता ही लहरा उठी हो-
प्रत्यग्रमज्जनविशेषविविक्तकान्तिःकौसुम्भरागरुचिरस्फुरदंशुकान्ता।
विभ्राजसे मकरकेतनमर्च्चयन्ती
बालप्रवालविटपिप्रभवा लतेव।
विभ्राजसे मकरकेतनमर्च्चयन्ती
बालप्रवालविटपिप्रभवा लतेव।
मालविकाग्नि मित्र से पता चलता है कि मदन देवता की पूजा के बाद ही अशोक में फूल खिला देने का अनुष्ठान होता था। रत्नावली में भी इसकी चर्चा है। इस अनुष्ठान का रूप इस प्रकार था-कोई सुन्दरी सर्वाभरण-भूषिता होकर, पैरों को अलक्तकराग से रंजित करके, नूपुर सहित बायें चरण से अशोक वृक्ष पर आघात करती थी। इधर नूपुरों की हल्की झनझनाहट, उधर अशोक का सोल्लास कंधे पर से ही फूल उठना। साधारणतः रानी यह कार्य करती थी। पर मालविकाग्निमित्र में बताया गया है कि उस रानी के पैरों में चोट आ गई थी, इसलिए उन्होंने मालविका को भेज दिया था। मालविका अशोक वृक्ष के पास गई, पल्लवों का गुच्छा हाथ से पकड़ा और बायें पैर से अशोक पर मृदु आघात किया। कालिदास की लेखनी ने इस मादक चित्र को अपूर्व गरिमा से भर दिया है।
परब्रह्म की उस मानसिक इच्छा का, जो संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होती है, मूर्तरूप ही ‘काम’ है। जब यह सृष्टि रचना के अनुकूल होती है तो विष्णु और शिव का साक्षात् रूप कही जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं जीवमात्र में धर्म के अविरुद्ध रहने वाला ‘काम’ हूँ, परन्तु जो व्यक्तिगत इच्छा धर्म के विरुद्ध जाती है, वह अपदेवता है। काम का एक रूप धर्म के अविरुद्ध जाने वाला है, दूसरा धर्म के विरुद्ध जाने वाला। पहला साक्षात् विष्णु रूप है। ब्रह्मसंहिता में कहा गया है कि जो आनन्द और चेतनामय रस से मन को भरता है, प्राणियों के मन में ‘स्मर’ या ‘काम’ रूप से प्रतिफलित होता है और इस प्रकार अशेष भुवनों की जीतकर नित्य विराजमान है, उस आदि- पुरुष गोविन्द को मैं स्मरण करता हूँ (46)। मत्स्यपुराण में ‘कामनाम्ना हरेरर्चां’ कहकर बताया गया है कि वस्तुतः ‘काम’ नामक हरि की ही पूजा की जाती है। इसलिए मंदिर और मूर्ति बनाकर जिस देवता की पूजा की जाती है, वह साक्षात् विष्णु ही हैं। श्री कृष्ण गायत्री और काम गायत्री में कोई फर्क नहीं है।
परब्रह्म की उस मानसिक इच्छा का, जो संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होती है, मूर्तरूप ही ‘काम’ है। जब यह सृष्टि रचना के अनुकूल होती है तो विष्णु और शिव का साक्षात् रूप कही जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं जीवमात्र में धर्म के अविरुद्ध रहने वाला ‘काम’ हूँ, परन्तु जो व्यक्तिगत इच्छा धर्म के विरुद्ध जाती है, वह अपदेवता है। काम का एक रूप धर्म के अविरुद्ध जाने वाला है, दूसरा धर्म के विरुद्ध जाने वाला। पहला साक्षात् विष्णु रूप है। ब्रह्मसंहिता में कहा गया है कि जो आनन्द और चेतनामय रस से मन को भरता है, प्राणियों के मन में ‘स्मर’ या ‘काम’ रूप से प्रतिफलित होता है और इस प्रकार अशेष भुवनों की जीतकर नित्य विराजमान है, उस आदि- पुरुष गोविन्द को मैं स्मरण करता हूँ (46)। मत्स्यपुराण में ‘कामनाम्ना हरेरर्चां’ कहकर बताया गया है कि वस्तुतः ‘काम’ नामक हरि की ही पूजा की जाती है। इसलिए मंदिर और मूर्ति बनाकर जिस देवता की पूजा की जाती है, वह साक्षात् विष्णु ही हैं। श्री कृष्ण गायत्री और काम गायत्री में कोई फर्क नहीं है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book