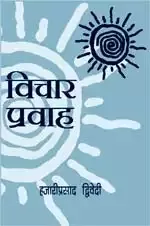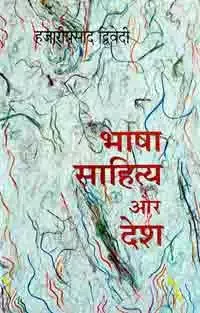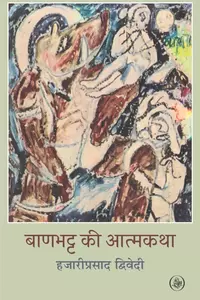|
लेख-निबंध >> विचार प्रवाह विचार प्रवाहहजारी प्रसाद द्विवेदी
|
10 पाठक हैं |
||||||
इस पुस्तक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मनुष्य जाति के प्रत्येक अनुभव और उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का आख्यान किया है...
Vichar pravah
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
विचार प्रवाह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबन्धों का महत्त्वपूर्ण संग्रह है। अपने निबन्धों के माध्यम से द्विवेदीजी मनुष्य जाति के प्रत्येक अनुभव, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धि और प्रकृति के हर विवर्तन का रेखांकन करते हैं। मनुष्य के विकासमान परम्परा-बोध और देश-कालगत परिस्थितियों में उनके मूल्यांकन की आवश्यकता पर उनका बराबर आग्रह रहा है। लोक-विमुख धर्म, दर्शन, साहित्य और कला-संस्कृति उनके लिए मूल्यहीन हैं। जड़ शास्त्रीयता से उनका गहरा विरोध है। यही कारण है कि द्विवेदीजी के कितने ही शोधपरक निबन्ध हमारे चेतन-अचेतन के वैचारिक कुहासे को छाँटने का कार्य करते हैं।
अपने ललित निबन्धों में द्विवेदीजी आद्यन्त कवि हैं। प्रकृति जैसे उसकी सहचरी बनकर आती है। अकुंठ भावोद्रेक और अप्रस्तुतों के भावोचित व्यंजक प्रयोग, सजीव बिम्बात्मकता और अपनी सहजता में बेजोड़ भाषा-शैली उनके इन निबन्धों को विश्वसाहित्य की अनमोल सम्पदा बना देती है। इनमें अवगाहन करता पाठक एक और आचार्यजी की कल्पनाशील भावप्रवणता से अभिभूत हो उठता है, तो दूसरी ओर ऐसे ज्ञान-कोश से परिचित होता है, जिसमें उदात्त जीवन-मूल्यों के राशि-राशि रत्न सुरक्षित हैं।
अपने ललित निबन्धों में द्विवेदीजी आद्यन्त कवि हैं। प्रकृति जैसे उसकी सहचरी बनकर आती है। अकुंठ भावोद्रेक और अप्रस्तुतों के भावोचित व्यंजक प्रयोग, सजीव बिम्बात्मकता और अपनी सहजता में बेजोड़ भाषा-शैली उनके इन निबन्धों को विश्वसाहित्य की अनमोल सम्पदा बना देती है। इनमें अवगाहन करता पाठक एक और आचार्यजी की कल्पनाशील भावप्रवणता से अभिभूत हो उठता है, तो दूसरी ओर ऐसे ज्ञान-कोश से परिचित होता है, जिसमें उदात्त जीवन-मूल्यों के राशि-राशि रत्न सुरक्षित हैं।
यह संस्करण
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रायः सभी कृतियाँ ‘राजकमल’ से प्रकाशित हैं। फिर भी कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो ‘राजकमल’ से बाहर है और लम्बे समय से अनुपलब्ध भी। हमारी हार्दिक इच्छा रही है कि ऐसी सभी कृतियों के नये संस्करण ‘राजकमल’ से प्रकाशित किये जायें। इस सन्दर्भ में हिन्दी साहित्यः उद्भव और विकास तथा सहज साधना का प्रकाशन उल्लेखनीय है और विचार प्रवाह का यह संस्करण भी हमारी इसी इच्छा का मूर्त रूप है। आशा है, आचार्य द्विवेदी की इस महत्त्वपूर्ण निबन्ध-कृति को नये रूप में पाकर पाठकों को सन्तोष होगा।
प्रकाशक
संस्कृत के महाकाव्यों की परम्परा
(1)
‘महाकाव्य’ शब्द का प्रयोग आजकल दो अर्थों में होने लगा है-अंग्रेजी के ‘एपिक’ शब्द के अर्थ में और प्राचीन आलंकारिक आचार्यों द्वारा प्रयुक्त सर्गबद्ध काव्य के अर्थ में। साधारणतः यूरोपियन पण्डितों ने भारतीय ‘एपिक’ कहकर केवल दो ग्रंथों की चर्चा की है, महाभारत की और रामायण की। भारतीय पण्डितों ने भी रामायण को आदिकाव्य कहा है, परन्तु महाभारत को ‘इतिहास’, ‘आख्यान’, ‘पाँचवाँ वेद’ आदि कहा है और इस प्रकार यह बताना चाहा है कि महाभारत रामायण से भिन्न श्रेणी की रचना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (1-5) के अनुसार इतिहास में पुराण और इतिवृत्त का समावेश होता है। ऐसा जान पड़ता है कि परवर्ती पुराणों की परम्परा महाभारत के रूप से सम्बद्ध है और काव्यों की परम्परा रामायण के रूप से; पर न तो परवर्ती पुराण महाभारत की ऊँचाई तक पहुँच सके हैं और न परवर्ती काव्य रामायण की गुरुता तक। महाभारत को यद्यपि ‘काव्य’ नहीं कहा गया तथापि उसमें कितने ही आख्यान ऐसे हैं जो निश्चित रूप से ‘काव्य’ की श्रेणी में आते हैं और समूचे महाभारत ने अपने विषय में कहा हैः ‘‘जैसे दही में मक्खन, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में आरण्यक, औषधों में अमृत, जलाशयों में समुद्र और चतुष्पदों में गौ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार इतिहास में यह ‘भारत’ श्रेष्ठ है।
इस आख्यान को सुनने के बाद अन्य कथाएँ उसी प्रकार फीकी मालूम होंगी जिस प्रकार कोकिल की वाणी सुनने के बाद काक की वाणी। जैसे पंचभूत से लोक की तीन संविधियाँ उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार इस इतिहास को सुनकर कवि-बुद्धियां उत्पन्न होती हैं।’’ यह बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि पिछले दो हजार वर्षों के भारतीय साहित्य को यह महाग्रंथ नित्य प्रेरित और चालित करता रहा है। अनेक युगों के संचित भारतीय ज्ञान का भण्डार माना जाता रहा है और ‘काव्य’ तो नहीं, पर :‘काव्य’ का प्रेरणा-दाता समझा जाता रहा है।
महाभारत की मूल कहानी कुरू-पाण्डव युद्ध है जो सम्भवतः प्राचीनतर कुरू-पाञ्चाल युद्ध का किञ्चित् परिवर्तित रूप था। परन्तु इस मूल कहानी के इर्द-गिर्द प्राचीन उपख्यान आ जुटे हैं, जिन्होंने इस ग्रंथ को संहिता’ (संग्रहीकृत) का रूप दिया है। इन कहानियों में से कई तो यूरोपियन देशों में इतनी प्रिय हुई हैं कि एक ही कहानी के, एक ही भाषा में तीन-तीन चार-चार अनुवाद हुए हैं। नल-दमयन्ती का उपख्यान ऐसा ही मोहक कथानक है जो मूल कथा से सम्बद्ध नहीं है पर यूरोप की भाषाओं में कई-कई बार अनूदित हो चुका है और भारतीय साहित्य के काव्यों और नाटकों को प्रेरणा दे सका है। उत्तरकालीन संस्कृति के अत्यन्त अलंकृत और अर्थगाम्भीर्य-पूर्ण महाकाव्य नैषध चरित का आधार यही उपख्यान है। ऐसे उपख्यानों को यूरोपियन पण्डितों ने ‘महाकाव्य के भीतर महाकाव्य’ एपिक विदिन एपिक) नाम दिया है।
सहृदय के चित को भाव-मथित कर डालने में ये उपख्यान अत्यन्त प्रभावशाली हैं। श्री एफ. वप्प जैसे मर्मोज्ञ विद्वान ने आज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले नल-दमयन्ती के उपख्यान की इस महिमा को अनुभव किया था। उन्होंने लिखा था, ‘‘मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी समझ में करुणा तथा आवेगों की दृष्टि से और भावों की समझ कोमलता तथा विमोहक शक्ति के खयाल से नल-दमयन्ती का उपाख्यान अद्वितीय है। इसकी रचना इस ढंग से की गयी है कि वह सबको आकर्षित करती है चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, उच्च जातीय हो या नीच जातीय, रसज्ञ आलोचक हो या सहज बुद्धि द्वारा चालित साधारण पाठक।’’ इस प्रकार नल के उपख्यान का प्रभाव विश्वजनीन है; वह मनुष्य के उस मर्मस्थल को स्पर्श करता है जो जाति और वाक्य तथा लिंग और धर्म के सभी आवरणों के नीचे अत्यन्त गहराई में हैं और जहाँ सभी मनुष्य एक है ‘साधारण’ हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि इस कि उपख्यान ने देश-विदेश के सहृदयों के चित्त को इस प्रकार आलोड़ित किया है और यह अनेक काव्यों और नाटकों का मूल प्रेरणादाता रहा है।
ऐसी कहानियाँ महाभारत में बहुत हैं। सावित्री-सत्यवान् के अख्यान के सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध जर्मन पंडित श्री विंटर नित्य ने लिखा था कि ‘‘चाहे जिस किसी ने सावित्री के काव्य की रचना की हो, चाहे कोई सूत रहा हो या ब्राह्मण, वह अवश्यमेव सब कालों का सर्वोच्च कवि था। कोई महान कवि ही इस उत्कृष्ट महिला-चरित्र को इतने मनमोहक एवं आकर्षक ढंग से चित्रित कर सकता था, और शुष्क उपदेश की मनोवृत्ति में पड़े बिना भाग्य और मृत्यु पर प्रेम तथा पातिवृत्य की विजय दिखला सकता था और प्रतिभाशाली कलाकार ही जादू की तरह ऐसे अश्चर्यजनक चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित कर सकता था।’’ ऐसी कहानियों का सीधा सम्बन्ध मूल कहानी से नहीं है पर मूल कहानी भी भारतवर्ष के और बाहर के सहृदयों और कवियों को शताब्दियों से प्रभावित करती रही है।
भारतवर्ष एक हाथ की रचना नहीं है। मूल ग्रन्थ से ही इस बात के प्रमाण खोजे गये हैं कि इस ग्रन्थ का सम्पादन एकाधिक बार किया गया है परन्तु एक हाथ की रचना पर भी महाभारत एक सम्पूर्ण युग की रचना है। इसमें किसी एक व्यक्ति का तो नहीं, पर एक सम्पूर्ण युग का व्याक्तित्व बहुत स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त हुआ है। इस युग में भारतीय जनता शहर और गाँव में जितनी अधिक नहीं बँट रही थी तो अन्तर बहुत थोड़ा था। अभिजात वंश के लोगों के साथ उसका अन्तर बहुत अधिक नहीं था। इस युग के राजा और सरदार लोगों ने हथियार नहीं छोड़ा था, वे साधारण जनता के साथ-साथ युद्ध में लड़ते थे और यदि राजवंश व्यक्ति साधारण व्यक्ति से प्रत्यक्ष वीरत्व में किसी प्राकार कम सिद्ध हुआ तो उसकी हेठी मानी जाती थी। महाभारत चरित्रों का विशाल वन है। इस ग्रंन्थ में ऐसे पात्र बहुत कम हैं- नहीं है कहना अधिक ठीक है जो महलों में पलकर चमके हों। सबके सब एक तूफान के भीतर से गुजरे हैं,
इस आख्यान को सुनने के बाद अन्य कथाएँ उसी प्रकार फीकी मालूम होंगी जिस प्रकार कोकिल की वाणी सुनने के बाद काक की वाणी। जैसे पंचभूत से लोक की तीन संविधियाँ उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार इस इतिहास को सुनकर कवि-बुद्धियां उत्पन्न होती हैं।’’ यह बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि पिछले दो हजार वर्षों के भारतीय साहित्य को यह महाग्रंथ नित्य प्रेरित और चालित करता रहा है। अनेक युगों के संचित भारतीय ज्ञान का भण्डार माना जाता रहा है और ‘काव्य’ तो नहीं, पर :‘काव्य’ का प्रेरणा-दाता समझा जाता रहा है।
महाभारत की मूल कहानी कुरू-पाण्डव युद्ध है जो सम्भवतः प्राचीनतर कुरू-पाञ्चाल युद्ध का किञ्चित् परिवर्तित रूप था। परन्तु इस मूल कहानी के इर्द-गिर्द प्राचीन उपख्यान आ जुटे हैं, जिन्होंने इस ग्रंथ को संहिता’ (संग्रहीकृत) का रूप दिया है। इन कहानियों में से कई तो यूरोपियन देशों में इतनी प्रिय हुई हैं कि एक ही कहानी के, एक ही भाषा में तीन-तीन चार-चार अनुवाद हुए हैं। नल-दमयन्ती का उपख्यान ऐसा ही मोहक कथानक है जो मूल कथा से सम्बद्ध नहीं है पर यूरोप की भाषाओं में कई-कई बार अनूदित हो चुका है और भारतीय साहित्य के काव्यों और नाटकों को प्रेरणा दे सका है। उत्तरकालीन संस्कृति के अत्यन्त अलंकृत और अर्थगाम्भीर्य-पूर्ण महाकाव्य नैषध चरित का आधार यही उपख्यान है। ऐसे उपख्यानों को यूरोपियन पण्डितों ने ‘महाकाव्य के भीतर महाकाव्य’ एपिक विदिन एपिक) नाम दिया है।
सहृदय के चित को भाव-मथित कर डालने में ये उपख्यान अत्यन्त प्रभावशाली हैं। श्री एफ. वप्प जैसे मर्मोज्ञ विद्वान ने आज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले नल-दमयन्ती के उपख्यान की इस महिमा को अनुभव किया था। उन्होंने लिखा था, ‘‘मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी समझ में करुणा तथा आवेगों की दृष्टि से और भावों की समझ कोमलता तथा विमोहक शक्ति के खयाल से नल-दमयन्ती का उपाख्यान अद्वितीय है। इसकी रचना इस ढंग से की गयी है कि वह सबको आकर्षित करती है चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, उच्च जातीय हो या नीच जातीय, रसज्ञ आलोचक हो या सहज बुद्धि द्वारा चालित साधारण पाठक।’’ इस प्रकार नल के उपख्यान का प्रभाव विश्वजनीन है; वह मनुष्य के उस मर्मस्थल को स्पर्श करता है जो जाति और वाक्य तथा लिंग और धर्म के सभी आवरणों के नीचे अत्यन्त गहराई में हैं और जहाँ सभी मनुष्य एक है ‘साधारण’ हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि इस कि उपख्यान ने देश-विदेश के सहृदयों के चित्त को इस प्रकार आलोड़ित किया है और यह अनेक काव्यों और नाटकों का मूल प्रेरणादाता रहा है।
ऐसी कहानियाँ महाभारत में बहुत हैं। सावित्री-सत्यवान् के अख्यान के सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध जर्मन पंडित श्री विंटर नित्य ने लिखा था कि ‘‘चाहे जिस किसी ने सावित्री के काव्य की रचना की हो, चाहे कोई सूत रहा हो या ब्राह्मण, वह अवश्यमेव सब कालों का सर्वोच्च कवि था। कोई महान कवि ही इस उत्कृष्ट महिला-चरित्र को इतने मनमोहक एवं आकर्षक ढंग से चित्रित कर सकता था, और शुष्क उपदेश की मनोवृत्ति में पड़े बिना भाग्य और मृत्यु पर प्रेम तथा पातिवृत्य की विजय दिखला सकता था और प्रतिभाशाली कलाकार ही जादू की तरह ऐसे अश्चर्यजनक चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित कर सकता था।’’ ऐसी कहानियों का सीधा सम्बन्ध मूल कहानी से नहीं है पर मूल कहानी भी भारतवर्ष के और बाहर के सहृदयों और कवियों को शताब्दियों से प्रभावित करती रही है।
भारतवर्ष एक हाथ की रचना नहीं है। मूल ग्रन्थ से ही इस बात के प्रमाण खोजे गये हैं कि इस ग्रन्थ का सम्पादन एकाधिक बार किया गया है परन्तु एक हाथ की रचना पर भी महाभारत एक सम्पूर्ण युग की रचना है। इसमें किसी एक व्यक्ति का तो नहीं, पर एक सम्पूर्ण युग का व्याक्तित्व बहुत स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त हुआ है। इस युग में भारतीय जनता शहर और गाँव में जितनी अधिक नहीं बँट रही थी तो अन्तर बहुत थोड़ा था। अभिजात वंश के लोगों के साथ उसका अन्तर बहुत अधिक नहीं था। इस युग के राजा और सरदार लोगों ने हथियार नहीं छोड़ा था, वे साधारण जनता के साथ-साथ युद्ध में लड़ते थे और यदि राजवंश व्यक्ति साधारण व्यक्ति से प्रत्यक्ष वीरत्व में किसी प्राकार कम सिद्ध हुआ तो उसकी हेठी मानी जाती थी। महाभारत चरित्रों का विशाल वन है। इस ग्रंन्थ में ऐसे पात्र बहुत कम हैं- नहीं है कहना अधिक ठीक है जो महलों में पलकर चमके हों। सबके सब एक तूफान के भीतर से गुजरे हैं,
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book