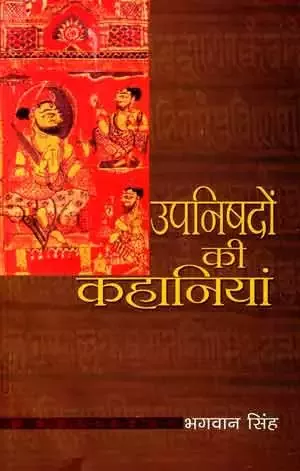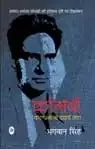|
विवेचनात्मक व उपदेशात्मक संग्रह >> उपनिषदों की कहानियाँ उपनिषदों की कहानियाँभगवान सिंह
|
432 पाठक हैं |
|||||||
वेद, पुराण, उपनिषद् आदि ऐसे सांसारिक ग्रन्थ हैं, जिनमें सदियों से हमारी सभ्यता के विकास का सम्यक् रूप संकलित है।
Upnishadon Ki Kahaniyan - A hindi Book by - Bhagwan Singh उपनिषदों की कहानियाँ - भगवान सिंह
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
वेद, पुराण, उपनिषद् आदि ऐसे सांसारिक ग्रन्थ हैं, जिनसे सदियों से हमारी सभ्यता के विकास का सम्यक् रूप संकलित है। प्राचीन काल की व्यक्ति कथा भी किस्सागोई के संयोग से कालांतर से विचित्र स्वरूप में आ गयी और भी ये ही सारी बातें बाद में दंतकथा, पुराणकथा, उपनिषद्-कथा और मिथक के रूप में जानी गयीं।
आज का साहित्य पुराने मिथक की नयी व्याख्या करने लगा है। प्रस्तुत पुस्तक उपनिषदों की कहानियों की नयी व्याख्या करती है। इनमें न केवल कहानियों का हू-ब-हू अनुवाद प्रस्तुत किया गया है, बल्कि जगह-ब-जगह उसकी कथा-उपकथा की खूबी-खामी की ओर संकेत करते हुए काफी मनोरंजक व्याख्या भी की गयी है। यह व्याख्या जहाँ एक ओर सामान्य पाठक का उपनिषद् की कहानियों से परिचय कराती है वहीं दूसरी ओर सदियों से व्याप्त वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की विरूपता पर व्यंग्य भी प्रस्तुत करती है।
इस पुस्तक के प्रस्तोता भगवान सिंह (जन्म 1931) हैं। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं- राम (कविता संकलन) काले उजले टीले, महाभिषग, अपने-अपने राम (उपन्यास), आर्य द्रविड़ भाषाओं की मूलभूत एकता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य (शोध ग्रन्थ)।
आज का साहित्य पुराने मिथक की नयी व्याख्या करने लगा है। प्रस्तुत पुस्तक उपनिषदों की कहानियों की नयी व्याख्या करती है। इनमें न केवल कहानियों का हू-ब-हू अनुवाद प्रस्तुत किया गया है, बल्कि जगह-ब-जगह उसकी कथा-उपकथा की खूबी-खामी की ओर संकेत करते हुए काफी मनोरंजक व्याख्या भी की गयी है। यह व्याख्या जहाँ एक ओर सामान्य पाठक का उपनिषद् की कहानियों से परिचय कराती है वहीं दूसरी ओर सदियों से व्याप्त वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की विरूपता पर व्यंग्य भी प्रस्तुत करती है।
इस पुस्तक के प्रस्तोता भगवान सिंह (जन्म 1931) हैं। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं- राम (कविता संकलन) काले उजले टीले, महाभिषग, अपने-अपने राम (उपन्यास), आर्य द्रविड़ भाषाओं की मूलभूत एकता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य (शोध ग्रन्थ)।
कहानीकारों का जमाना
यह जमाना बीसवीं शताब्दी से उतना ही दूर था जितना सुपरसोनिक से गधा। रफ्तार भी वही। हर चीज ढीली-ढाली थी, और लोग देखने में गंवार से लगते थे। दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए, विचार उलझे हुए। पर वे बीसवीं शताब्दी के लोगों की ओर उंगली उठा कर कह रहे थे, उन मूर्खों को देखो। वे अधिक खाने के लोभ में अपने समुद्र और आसमान तक को खाते जा रहे हैं। अपने भविष्य को खाते जा रहे हैं और, फिर भी, अपने को विज्ञानी समझते हैं। वे हजारों साल की दूरी के आस-पास देख रहे थे, जैसे समय भी उनके लिए किसी मैदान की तरह सपाट हो। उनके इस उपहास को सुन कर अपनी शताब्दी के ज्ञान पर गरूर करने वाला मैं शर्म से सिर तक नहीं उठा पा रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं सचमुच रैक्वजाद बिरादरी में शामिल हो गया हूं। उनके इस तरह हंसने का कुछ अधिकार भी था, क्योंकि उनकी नदियां सिर्फ बरसात में मैली होती थीं, उनका आसमान सिर्फ आंधी चलने पर मैला होता था, उनकी धूप केवल बादल घिरने पर मैली होती थी, उनके विचार केवल आवेग की प्रखरता में मैले होते थे, उनका शरीर केवल काम करते समय मैला होता था, उनकी आत्मा तो मैली होती ही नहीं थी। वे हंसते थे तो उनकी हंसी में उनका आह्लाद झलकता था, दर्प झलकता था, व्यंग्य झलकता था, पर मन की मलिनता नहीं झलतती थी। वह उनके दिल दिमाग में कहीं थी ही नहीं।
वे बहुत कम दुखी होते थे, क्योंकि दुख की उनकी परिभाषा भिन्न थी। हमारी परिभाषा के बहुत से दुखों को वे चुपचाप पी जाते थे, मानो वह दुख हो ही नहीं। पर जब दुख उनकी परिभाषा के अनुसार भी दुख बन जाता था तो उससे आंसू के स्थान पर दर्शन टपकने लगता था।
उनके चेहरे पर ज्ञान तेज और तुष्टि बन कर झलकता था। उनकी जरूरतें बहुत कम थीं। वे सब कुछ अपने लिए नहीं चाहते थे। पेट भरने के बाद उनकी भूख तेज नहीं होती थी। वे बहुत कम चीजों से डरते थे, बहुत अधिक चीजों पर भरोसा करते थे और घृणा तो किसी चीज से करते ही नहीं थे।
उस युग में सोचने के काम में सोचने में माहिर लोगों के साथ उन लोगों ने सहयोग करना शुरू कर दिया था जो अब तक सारे काम बिना सोचे बिचारे, सीना जोरी से करते आए थे। आदत के मुताबिक उन्होंने सोचने का काम भी सीनाजोरी से ही करना शुरू किया। पहले से चले आ रहे विचारों और विश्वासों को वे ऐसे उलट-पलट रहे थे कि लगता था कोई चीज अपनी सही जगह पर रह ही नहीं पाएगी। वे कहते थे, वेद वेद नहीं है, यज्ञ यज्ञ नहीं है, ज्ञान ज्ञान नहीं है, संसार संसार नहीं है, पराया पराया नहीं है, अपना अपना नहीं है। उनके ज्ञान के साधन बहुत सीमित और अविश्वसनीय थे, पर वे जो कुछ सोचते थे बहुत साफ सोचते थे क्योंकि वे निडर हो कर सोचते थे।
सोचने के काम में जुटने वाले इन नवचिंतकों के लिए सोचने का काम नया-नया था, इसलिए वे बहुत जोर लगा कर सोच रहे थे और लगातार सोचते ही चले जा रहे थे। वे खुद भी नहीं जानते थे कि इतना सोच कर वे करेंगे क्या और अपने ओजस्वी विचारों को रखेंगे कहां। उनके साथ एक परेशानी यह थी कि वे अपने विचारों को ठोस बनाने के लाख जतन करते पर वे बार-बार अमूर्त हो जाते थे। इन्हें ठोस बनाने के लिए वे बात-बात में कहानियां और कविताएं, पहेलियां और उलटबांसियां गढ़ते थे। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए धरती से आकाश तक दौड़ते फिरते थे और जिस तिस को पकड़ लेते थे, पर बात कुछ ऐसी थी कि बार-बार कहने पर अनकही रह जाती थी। ठोस बनाने की कोशिश में भी अठोस हो जाती थी। समझ में आते हुए भी समझ में नहीं आती थी और इसे मानते हुए भी कोई इस तरह नहीं मानता था कि इसे न मानना न कहा जा सके। उनको अपनी बात को वजनी बनाने का शौक था। उनका विश्वास था कि किसी विचार का वजन इस बात से नापा जा सकता है कि उसे समझने में किसी को कितना समय लगता है और इस होड़ में वे अपनी बातों को इतना घुमा फिरा कर या दुरुह बना कर रखते थे कि उसका पार पाने के लिए सहस्राब्दियां भी काफी नहीं थीं।
वे कुछ जानने के लिए नहीं सोचते थे। जाने हुए का आनंद लेने के लिए सोचते थे। उसे जीवन में उतारने के लिए सोचते थे। सोचते रहने के लिए सोचते थे। उन लोगों को दुनिया की हर बात मालूम थी। जो हो चुकी थी वह भी, जो होने वाली थी वह भी, और जो नहीं हो सकती थी वह भी। उनकी आँखों के आगे तीनों काल और सातों लोक आंख झपकते ही खुल जाते थे।
देखने का उनका तरीका भी कुछ कम अजीब नहीं था। हमें कुछ देखना होता है तो हम आंख फाड़-फाड़ कर, चश्मे, दूरबीन और खुर्दबीन लगा कर देखते हैं और वे देखने के लिए आंख बंद कर लेते थे। उनमें से जानकार लोगों का मानना था कि ब्रह्मांड बाहर नहीं है। सारा ब्रह्माडं उनके भीतर भरा हुआ है। काल उनके भीतर सिमटा हुआ है। बाहर तो मात्र उसकी छाया है। यह आसान सी बात भी इतनी गूढ़ थी कि इसे समझने के लिए गुरु का होना और उसके मुंह से इसे सुनना जरूरी था। उनकी आंख कुछ इस तरह बनी थी कि पलक झपकते ही उनकी पुतलियां बाहर से भीतर की ओर लौट जाती थीं और कोई चीज दुनिया में कहां है, क्यों है, है या नहीं, है, होगी या नहीं होगी, यह सब उन्हें दिखाई देने लगता था।
उनकी ज्ञानमीमांसा में ज्ञान ज्ञान नहीं था, परले दरजे का अज्ञान था। उनका मानना था कि इससे आदमी आदमी की तरह रहने की जगह चालाक जानवरों की तरह रहने लगता है। बहुत अधिक खाता है, बहुत अधिक पीता है, बहुत अधिक भोगता है, इंद्रियों का बहुत अधिक गुलाम बनता जाता है और जीवन मरण के चक्र में बहुत अधिक उलझता जाता है। वह अपनी चालाकी में भी मूर्खता ही करता है, क्योंकि कालदेव के लिए अपने शरीर को बकरे की तरह पाल कर मोटा करने के अतिरिक्त वह और क्या करता है ? असली ज्ञान तो जीवन और जगत के प्रति सही दृष्टिकोण है।
एक विचित्र बात यह थी कि उन्हें अज्ञान से भी उतना ही प्रेम था जितना ज्ञान से था। वे कहते थे अविद्या या भौतिक ज्ञान से केवल जीवन निर्वाह होता है केवल मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। वास्तविक आनंद और मुक्ति तो विद्या में है। इस बोध में है कि समस्त ब्रह्मांड हमारे भीतर है और हम ही समस्त ब्रह्मांड में हैं। इस ब्रह्मांड को क्षति पहुंचा कर हम अपने को क्षति पहुंचाते हैं। यह विश्व हम में है और इस विश्व में हम हैं। वे कहते थे इस दुनिया में शत्रु भाव से न रहो। मैत्री से रहना सीखो।
वे कहानीकार नहीं थे पर कहानी गढ़ रहे थे। कहानी गढ़ने का उनका तरीका भी शानदार था। शब्दों की जगह वे जीते-जागते पात्रों को उठा लाते और फिर उनसे जो चाहते कहलवा लेते, जैसा चाहते करा लेते और इसके बाद उन्हें इस तरह उठा कर फेंक देते थे कि पात्रों की हड्डियों का चटकना तक सुनाई देता था।
वे कहानीकार कहाने के लिए कहानियां नहीं कह रहे थे। वे कहानी कहे बिना रह नहीं पाते थे। पर ऐसे कहानीकार जो अनचाहे कहानी कहने चले हों, कहानी के साथ कुछ नया गुल तो खिलाएंगे ही। कहानी व्यक्ति की होती है। इनको कहानी उसकी कहने की पड़ी थी जो समाष्टि के सार का भी अमूर्तन है। उन्होंने कहानी के तकाजे से उसे पुरुष और प्रजापति बना दिया। अब ये ऐसे धाकड़ कहानीकार बन गए जो अनुभूत सच को बदल कर कहानी के अनुरूप एक नया सच गढ़ लेते थे और गढ़ते समय इस बात से गाफिल बने रहते थे कि वे कुछ गढ़ भी रहे हैं। नाम तो उन्होंने उन्हें पुरुष का दिया और हाल यह कि नाक-नक्श नदारद। आधी समस्या तो उस पुरुष का पता मालूम करने की थी जो है भी, और नहीं भी है। बाकी आधी उसकी शिनाख्त करने की थी, जो निराकार तो है, पर इतना निराकार भी नहीं कि उसे आकारहीन कहा जा सके। दुनिया की किसी पुलिस का पाला इतने बड़े गुनहगार से न पड़ा होगा जिसके गुनाहों का फल सबको भोगना पड़ रहा हो और फिर भी जिसके छिपने के अड्डे और भेस बदलने के तरीके इतने नायाब हों कि जहां उसके होने का शर्तिया पता हो वहां पहुंचने पर वह गायब मिले। जिसे पहचान कर उसे पकड़ लीजिए उस पर नजर डालते ही कहना पड़े, ‘‘क्षमा कीजिएगा, गलती हो गई।’’
अगर वे खांटी कहानीकार होते तो इतना बड़ा जोखिम न उठाते। कहानीकार कुछ फितरती और काइयां किस्म का जीव होता है जो शहद भी कुछ इस अदा से चाटता है कि देखने वाले को लगे वह ततैया के छत्ते में मुंह मार रहा है। और फिर वह दुनियादार भी खासा होता है। वह सोचता कम है, पर सोचता हुआ दिखता अधिक है। लिखता कम है पर उस लिखे को बेचने का ढेर सारा इंतजाम कर लेता है।
वे विचारों को कहानी और कहानी को कविता और कहानी और कविता दोनों को घोंट-पीस कर ब्रह्मत्व बना रहे थे। इससे एक नई विधा पैदा हो रही थी जिसे बूझो तो बताएं विधा कहा जा सकता है। वे ऐसे लोगों के लिए मसाला तैयार कर रहे थे जो पाठशाला से इतनी दूर रखे जाते थे कि उनके शरीर का स्पर्श करने से अपवित्र हुई हवा तक पाठशाला में प्रवेश न कर सके।
उनकी कहानियां अकहानी विधा की आदि कहानियां थीं। कोई किस्सागो यदि इन कहानियों को सुनाने चलता तो श्रोता कहानी आरंभ होने से पहले ही ऊंघना शुरू कर देता। इससे इन कहानियों का नुकसान नहीं हुआ। उनका तो फायदा ही हुआ है। श्रोताओं की ऊंघ और झपकी के प्रताप से बार-बार कही और सुनी जाने के बाद भी कहने सुनने वालों का जो भी हुआ हो, इन कहानियों का कुछ नहीं बिगड़ा इन्हें बहुतों ने सुनते हुए भी नहीं सुना, पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ा, और जानते हुए भी नहीं जाना। उनकी कविताएं बार-बार पढ़ी गई हैं, पर वे आज भी प्राणवायु की तरह स्फूर्तिदायक बनी रह गई हैं। उनका दर्शन आज भी इतना प्राणवान है कि लगता है, इसे हमारे युग के गंभीर सवालों को ही ले कर लिखा गया है।
वे दुनिया की चिंता न करते हुए भी अपनी दुनिया से अधिक हमारी दुनिया के बारे में सोच रहे थे-पर्यावरण के ध्वंस पर, प्राकृतिक साधनों के अपव्यय पर, उपभोक्ता संस्कृति की विकृतियों पर, विज्ञान के पागलपन पर, मानवमूल्यों के ह्रास पर, संवेदन शून्यता की विडंबना पर और भाषा के दुष्प्रयोग पर। इस दृष्टि से वे आज के महान से महान वैज्ञानिक की तुलना में भी अधिक दूरदर्शी थे। इन्हीं कहानियों को पढ़ते हुए दुनिया से होते हुए अपनी दुनिया में प्रवेश करने का छोटा रास्ता निकालने की एक कोशिश हम यहां करने जा रहे हैं। इसमें सफल हो पाते हैं या नहीं, यह तो आगे चल कर ही पता चलेगा।
एक बात तय है। जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं और जिस पर एक भारतीय के नाते हमें सचमुच गर्व है उसकी प्राणवायु उनका चिंतन ही है। धार्मिक कट्टरता के आज के युग में यह जानना सुखद हो सकता है कि वे धर्म को निष्ठा और मानवीय अनुराग से अलग करके नहीं देखते थे। वे अपने से भिन्न मत और विचार के व्यक्तियों को भी अपना ही रूप मानते थे। वे जानते थे कि इससे मनुष्य किसी से घृणा नहीं करता। वे धार्मिक कट्टरता से पैदा होने वाली घृणा को ही नहीं पहचानते थे अपितु इस घृणा से बाहर आने का रास्ता भी जानते थे :
वे बहुत कम दुखी होते थे, क्योंकि दुख की उनकी परिभाषा भिन्न थी। हमारी परिभाषा के बहुत से दुखों को वे चुपचाप पी जाते थे, मानो वह दुख हो ही नहीं। पर जब दुख उनकी परिभाषा के अनुसार भी दुख बन जाता था तो उससे आंसू के स्थान पर दर्शन टपकने लगता था।
उनके चेहरे पर ज्ञान तेज और तुष्टि बन कर झलकता था। उनकी जरूरतें बहुत कम थीं। वे सब कुछ अपने लिए नहीं चाहते थे। पेट भरने के बाद उनकी भूख तेज नहीं होती थी। वे बहुत कम चीजों से डरते थे, बहुत अधिक चीजों पर भरोसा करते थे और घृणा तो किसी चीज से करते ही नहीं थे।
उस युग में सोचने के काम में सोचने में माहिर लोगों के साथ उन लोगों ने सहयोग करना शुरू कर दिया था जो अब तक सारे काम बिना सोचे बिचारे, सीना जोरी से करते आए थे। आदत के मुताबिक उन्होंने सोचने का काम भी सीनाजोरी से ही करना शुरू किया। पहले से चले आ रहे विचारों और विश्वासों को वे ऐसे उलट-पलट रहे थे कि लगता था कोई चीज अपनी सही जगह पर रह ही नहीं पाएगी। वे कहते थे, वेद वेद नहीं है, यज्ञ यज्ञ नहीं है, ज्ञान ज्ञान नहीं है, संसार संसार नहीं है, पराया पराया नहीं है, अपना अपना नहीं है। उनके ज्ञान के साधन बहुत सीमित और अविश्वसनीय थे, पर वे जो कुछ सोचते थे बहुत साफ सोचते थे क्योंकि वे निडर हो कर सोचते थे।
सोचने के काम में जुटने वाले इन नवचिंतकों के लिए सोचने का काम नया-नया था, इसलिए वे बहुत जोर लगा कर सोच रहे थे और लगातार सोचते ही चले जा रहे थे। वे खुद भी नहीं जानते थे कि इतना सोच कर वे करेंगे क्या और अपने ओजस्वी विचारों को रखेंगे कहां। उनके साथ एक परेशानी यह थी कि वे अपने विचारों को ठोस बनाने के लाख जतन करते पर वे बार-बार अमूर्त हो जाते थे। इन्हें ठोस बनाने के लिए वे बात-बात में कहानियां और कविताएं, पहेलियां और उलटबांसियां गढ़ते थे। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए धरती से आकाश तक दौड़ते फिरते थे और जिस तिस को पकड़ लेते थे, पर बात कुछ ऐसी थी कि बार-बार कहने पर अनकही रह जाती थी। ठोस बनाने की कोशिश में भी अठोस हो जाती थी। समझ में आते हुए भी समझ में नहीं आती थी और इसे मानते हुए भी कोई इस तरह नहीं मानता था कि इसे न मानना न कहा जा सके। उनको अपनी बात को वजनी बनाने का शौक था। उनका विश्वास था कि किसी विचार का वजन इस बात से नापा जा सकता है कि उसे समझने में किसी को कितना समय लगता है और इस होड़ में वे अपनी बातों को इतना घुमा फिरा कर या दुरुह बना कर रखते थे कि उसका पार पाने के लिए सहस्राब्दियां भी काफी नहीं थीं।
वे कुछ जानने के लिए नहीं सोचते थे। जाने हुए का आनंद लेने के लिए सोचते थे। उसे जीवन में उतारने के लिए सोचते थे। सोचते रहने के लिए सोचते थे। उन लोगों को दुनिया की हर बात मालूम थी। जो हो चुकी थी वह भी, जो होने वाली थी वह भी, और जो नहीं हो सकती थी वह भी। उनकी आँखों के आगे तीनों काल और सातों लोक आंख झपकते ही खुल जाते थे।
देखने का उनका तरीका भी कुछ कम अजीब नहीं था। हमें कुछ देखना होता है तो हम आंख फाड़-फाड़ कर, चश्मे, दूरबीन और खुर्दबीन लगा कर देखते हैं और वे देखने के लिए आंख बंद कर लेते थे। उनमें से जानकार लोगों का मानना था कि ब्रह्मांड बाहर नहीं है। सारा ब्रह्माडं उनके भीतर भरा हुआ है। काल उनके भीतर सिमटा हुआ है। बाहर तो मात्र उसकी छाया है। यह आसान सी बात भी इतनी गूढ़ थी कि इसे समझने के लिए गुरु का होना और उसके मुंह से इसे सुनना जरूरी था। उनकी आंख कुछ इस तरह बनी थी कि पलक झपकते ही उनकी पुतलियां बाहर से भीतर की ओर लौट जाती थीं और कोई चीज दुनिया में कहां है, क्यों है, है या नहीं, है, होगी या नहीं होगी, यह सब उन्हें दिखाई देने लगता था।
उनकी ज्ञानमीमांसा में ज्ञान ज्ञान नहीं था, परले दरजे का अज्ञान था। उनका मानना था कि इससे आदमी आदमी की तरह रहने की जगह चालाक जानवरों की तरह रहने लगता है। बहुत अधिक खाता है, बहुत अधिक पीता है, बहुत अधिक भोगता है, इंद्रियों का बहुत अधिक गुलाम बनता जाता है और जीवन मरण के चक्र में बहुत अधिक उलझता जाता है। वह अपनी चालाकी में भी मूर्खता ही करता है, क्योंकि कालदेव के लिए अपने शरीर को बकरे की तरह पाल कर मोटा करने के अतिरिक्त वह और क्या करता है ? असली ज्ञान तो जीवन और जगत के प्रति सही दृष्टिकोण है।
एक विचित्र बात यह थी कि उन्हें अज्ञान से भी उतना ही प्रेम था जितना ज्ञान से था। वे कहते थे अविद्या या भौतिक ज्ञान से केवल जीवन निर्वाह होता है केवल मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। वास्तविक आनंद और मुक्ति तो विद्या में है। इस बोध में है कि समस्त ब्रह्मांड हमारे भीतर है और हम ही समस्त ब्रह्मांड में हैं। इस ब्रह्मांड को क्षति पहुंचा कर हम अपने को क्षति पहुंचाते हैं। यह विश्व हम में है और इस विश्व में हम हैं। वे कहते थे इस दुनिया में शत्रु भाव से न रहो। मैत्री से रहना सीखो।
वे कहानीकार नहीं थे पर कहानी गढ़ रहे थे। कहानी गढ़ने का उनका तरीका भी शानदार था। शब्दों की जगह वे जीते-जागते पात्रों को उठा लाते और फिर उनसे जो चाहते कहलवा लेते, जैसा चाहते करा लेते और इसके बाद उन्हें इस तरह उठा कर फेंक देते थे कि पात्रों की हड्डियों का चटकना तक सुनाई देता था।
वे कहानीकार कहाने के लिए कहानियां नहीं कह रहे थे। वे कहानी कहे बिना रह नहीं पाते थे। पर ऐसे कहानीकार जो अनचाहे कहानी कहने चले हों, कहानी के साथ कुछ नया गुल तो खिलाएंगे ही। कहानी व्यक्ति की होती है। इनको कहानी उसकी कहने की पड़ी थी जो समाष्टि के सार का भी अमूर्तन है। उन्होंने कहानी के तकाजे से उसे पुरुष और प्रजापति बना दिया। अब ये ऐसे धाकड़ कहानीकार बन गए जो अनुभूत सच को बदल कर कहानी के अनुरूप एक नया सच गढ़ लेते थे और गढ़ते समय इस बात से गाफिल बने रहते थे कि वे कुछ गढ़ भी रहे हैं। नाम तो उन्होंने उन्हें पुरुष का दिया और हाल यह कि नाक-नक्श नदारद। आधी समस्या तो उस पुरुष का पता मालूम करने की थी जो है भी, और नहीं भी है। बाकी आधी उसकी शिनाख्त करने की थी, जो निराकार तो है, पर इतना निराकार भी नहीं कि उसे आकारहीन कहा जा सके। दुनिया की किसी पुलिस का पाला इतने बड़े गुनहगार से न पड़ा होगा जिसके गुनाहों का फल सबको भोगना पड़ रहा हो और फिर भी जिसके छिपने के अड्डे और भेस बदलने के तरीके इतने नायाब हों कि जहां उसके होने का शर्तिया पता हो वहां पहुंचने पर वह गायब मिले। जिसे पहचान कर उसे पकड़ लीजिए उस पर नजर डालते ही कहना पड़े, ‘‘क्षमा कीजिएगा, गलती हो गई।’’
अगर वे खांटी कहानीकार होते तो इतना बड़ा जोखिम न उठाते। कहानीकार कुछ फितरती और काइयां किस्म का जीव होता है जो शहद भी कुछ इस अदा से चाटता है कि देखने वाले को लगे वह ततैया के छत्ते में मुंह मार रहा है। और फिर वह दुनियादार भी खासा होता है। वह सोचता कम है, पर सोचता हुआ दिखता अधिक है। लिखता कम है पर उस लिखे को बेचने का ढेर सारा इंतजाम कर लेता है।
वे विचारों को कहानी और कहानी को कविता और कहानी और कविता दोनों को घोंट-पीस कर ब्रह्मत्व बना रहे थे। इससे एक नई विधा पैदा हो रही थी जिसे बूझो तो बताएं विधा कहा जा सकता है। वे ऐसे लोगों के लिए मसाला तैयार कर रहे थे जो पाठशाला से इतनी दूर रखे जाते थे कि उनके शरीर का स्पर्श करने से अपवित्र हुई हवा तक पाठशाला में प्रवेश न कर सके।
उनकी कहानियां अकहानी विधा की आदि कहानियां थीं। कोई किस्सागो यदि इन कहानियों को सुनाने चलता तो श्रोता कहानी आरंभ होने से पहले ही ऊंघना शुरू कर देता। इससे इन कहानियों का नुकसान नहीं हुआ। उनका तो फायदा ही हुआ है। श्रोताओं की ऊंघ और झपकी के प्रताप से बार-बार कही और सुनी जाने के बाद भी कहने सुनने वालों का जो भी हुआ हो, इन कहानियों का कुछ नहीं बिगड़ा इन्हें बहुतों ने सुनते हुए भी नहीं सुना, पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ा, और जानते हुए भी नहीं जाना। उनकी कविताएं बार-बार पढ़ी गई हैं, पर वे आज भी प्राणवायु की तरह स्फूर्तिदायक बनी रह गई हैं। उनका दर्शन आज भी इतना प्राणवान है कि लगता है, इसे हमारे युग के गंभीर सवालों को ही ले कर लिखा गया है।
वे दुनिया की चिंता न करते हुए भी अपनी दुनिया से अधिक हमारी दुनिया के बारे में सोच रहे थे-पर्यावरण के ध्वंस पर, प्राकृतिक साधनों के अपव्यय पर, उपभोक्ता संस्कृति की विकृतियों पर, विज्ञान के पागलपन पर, मानवमूल्यों के ह्रास पर, संवेदन शून्यता की विडंबना पर और भाषा के दुष्प्रयोग पर। इस दृष्टि से वे आज के महान से महान वैज्ञानिक की तुलना में भी अधिक दूरदर्शी थे। इन्हीं कहानियों को पढ़ते हुए दुनिया से होते हुए अपनी दुनिया में प्रवेश करने का छोटा रास्ता निकालने की एक कोशिश हम यहां करने जा रहे हैं। इसमें सफल हो पाते हैं या नहीं, यह तो आगे चल कर ही पता चलेगा।
एक बात तय है। जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं और जिस पर एक भारतीय के नाते हमें सचमुच गर्व है उसकी प्राणवायु उनका चिंतन ही है। धार्मिक कट्टरता के आज के युग में यह जानना सुखद हो सकता है कि वे धर्म को निष्ठा और मानवीय अनुराग से अलग करके नहीं देखते थे। वे अपने से भिन्न मत और विचार के व्यक्तियों को भी अपना ही रूप मानते थे। वे जानते थे कि इससे मनुष्य किसी से घृणा नहीं करता। वे धार्मिक कट्टरता से पैदा होने वाली घृणा को ही नहीं पहचानते थे अपितु इस घृणा से बाहर आने का रास्ता भी जानते थे :
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विजुगुप्सते।।
सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विजुगुप्सते।।
वे कह रहे थे कि जो असंभूति या देवताओं या पितरों या मनुष्यों की उपासना करता है वह घोर अंधकार में पड़ जाता है, परंतु जो गुमान में रहता कि वह तो सर्वोपरि सत्ता की उपासना करता है वह इससे भी अधिक अंधकार में है। बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के उपासकों की जड़ता को पहचानते हुए वे कह रहे थे कि ईश्वर से प्रेम नहीं, मनुष्य से प्रेम करना सीखो। प्रकाश का, समझदारी का रास्ता यही है। देवताओं और पुजारियों के चक्कर में पड़ोगे। तो स्वयं तो बहकोगे ही दूसरों को भी बहकाओगे। मनुष्यों से प्यार करने के स्थान पर उनसे घृणा करने लगोगे और फिर अपने आप से भी घृणा करने लगोगे क्योंकि दूसरों से प्रेम करना अंततः अपने आप से प्रेम करना है और दूसरों से घृणा अपने आपसे भी घृणा करने का ही पर्याय है।
अंधं तम: प्रविशंति ये असंभूर्ति उपासते।
ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रता:।।
ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रता:।।
वे कह रहे थे कि संसार में ऐसा तो कुछ है ही नहीं जिसमें ईश्वर का निवास न हो। उसे पाने के लिए किसी देवालय या मस्जिद या गुरुद्वारे या गिरजा में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सच्चा मानव प्रेम ही काफी है। पर यह मानव प्रेम खोखला प्रेम नहीं है। यह तुम्हारे आचार से जुड़ा है और इस आचार का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक है। तुम त्यागपूर्वक भोग करो। अपने पास अतिरिक्त संचय न करो। लोभ में अंधे न बनो। पैसा किसी का हुआ नहीं है :
ईशा वास्यं इदं सर्वं यत् किं च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध: कस्य स्विद् धनम्।।
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध: कस्य स्विद् धनम्।।
हमारी अधिकांश धार्मिक ग्रंथियों और पारस्परिक कटुता का कारण यह है कि हम धर्म को कर्म से अलग कर लेते हैं। घटिया से घटिया आचरण करते हुए या निठल्ले पन की जिंदगी जीते हुए धर्म के नाम पर कुछ मिनटों की पूजा, पाठ या नमाज करके छुट्टी पा लेते हैं और शेष शक्ति को अपने धर्म की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए दूसरे धर्मों और विश्वासों से घृणा करने में प्रकट करते हैं। यह सोचते भी नहीं कि ये सभी मनुष्य के पतन में सहायक होते हैं। वे इसके स्थान पर आजीवन सच्चे मन से काम करते रहने का सुझाव दे रहे थे क्योंकि पवित्रता, मानवीय निष्ठा और धार्मिक निष्ठा सभी की कसौटी यही है। यदि इस विचार की महत्ता को ठीक वही स्थान मिले तो न तो कहीं धार्मिक विद्वेष दिखाई दे, न धार्मिक भेद और धर्मनिष्ठा स्वयं भौतिक और नैतिक विकास का सोपान बन जाए :
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा:।
एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।
एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।
ये कहानियां उपनिषदों की ही हैं। परन्तु इन्हें प्रस्तुत करने में यथेष्ट छूट ली गई है। आशा है पाठकों को यह रूप भी तोषप्रद लगेगा।
भगवान सिंह
रैक्व की कथा
जानश्रुत पौत्रायण बड़ा उदार था। बहुत दानी। भंडारा चलता रहता उसके यहां। कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, किसी भी जाति का हो। चारों ओर उसके नाम की धूम मची थी। उसने जगह-जगह आवसथ या धर्मशालाएं बनवा रखी थीं जहां सदावर्त चलता रहता था। वह चाहता था कि सभी लोग उसका दिया हुआ अन्य ही खाएं।
दान पुण्य से एक खास तरह का तेज पैदा होता है। यह आंखों से तो दिखाई नहीं देता पर इसका प्रभाव सब पर प्रकट होता रहता है। उसका तेज द्युलोक तक फैला हुआ था। उसे स्पर्श करने वाला, उससे स्पर्धा करने वाला, उस तेज से ही भस्म हो सकता था। जैसे चंद्रमा की किरणें दिन में नहीं दिखाई देतीं उसी तरह यह तेज सभी को दिखाई नहीं देता था, पर रात के समय प्रखर दृष्टि रखने वालों को दिखाई दे जाता था। आकाश में यह तेज जिस ऊंचाई तक फैला हुआ था उस ऊंचाई तक आदमी अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकता था। सो रात में आकाश में उड़ते हुए हंसों ने इस तेज को देखा। उनमें से एक हंस ने दूसरे से हंस कर कहा, ‘देखो तो जानश्रुति का तेज आकाश में किस तरह फैला हुआ है। इससे बच कर चलना नहीं तो भस्म हो जाओगे।’’ पर जिस हंस से यह बात कही गई थी उसका सामान्य ज्ञान सलाह देने वाले हंस से अधिक अच्छा था। उसने कहा, ‘‘तुम जानश्रुति पौत्रायण की तारीफ इसलिए कर रहे हो कि तुमको छकड़ेवाले रैक्व के बारे में कुछ पता ही नहीं।’’
अब पहले को जिज्ञासा हुई, छकड़ेवाले रैक्व में ऐसी क्या खास बात है ?
दूसरे हंस ने कहा, ‘‘जुए के खेल में जैसे कृत के पासे के सामने दूसरे सभी पासे ओछे पड़ते हैं और उन पर बदा गया दांव उस खिलाड़ी को मिल जाता है जिसका कृत आ जाता है उसी तरह दूसरे लोग जो भी सत्कर्म करते हैं उसका पुण्य रैक्व के पास पहुंच जाता है। इसकी वजह यह है कि रैक्व जिस विद्या को जानता है उसे कोई नहीं जानता।’’
पौत्रायण को सभी पक्षियों की भाषा न भी मालूम रही हो तो भी हंसों की भाषा तो मालूम थी ही। लगता है उसे अनिद्रा की बीमारी भी थी। हंस अपनी उड़ान रात में ही भरते हैं। वे शुद्ध आत्मा होते हैं इसलिए वे झूठ नहीं बोलते, यह तो सभी जानते हैं। पौत्रायण को उनकी बात पर बहुत भरोसा था। उसने हंसों की बातचीत सुनी तो वह उनकी बात का कायल भी हो गया।
उसके अगले दिन चारणों ने जब उसकी स्तुति आरंभ की तो उसने कहा, ‘‘तुम लोग मेरी स्तुति तो इस तरह कर रहे हो मानो मैं छकड़ेवाला रैक्व होऊं।’’
इस पर उन चारणों को भी रैक्व के विषय में उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा, ‘‘महाराज यह छकड़ेवाला रैक्व कौन है ?’’
राजा ने उन हंसों की बात उन्हें बता दी।
पौत्रायण ने सोचा यदि रैक्व सचमुच इतना तेजस्वी है तो उसका पता लगाना चाहिए और उससे वह विद्या जाननी चाहिए। उसने चारों ओर अपने चर दौड़ाए। रैक्व की तलाश शुरू हुई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस महाप्रतापी की यह महिमा बताई गई है वे गाड़ी के नीचे दुबके बैठे हो सकते हैं, इसलिए रैक्व पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी। एक-एक कर सभी चर लौट आए और उन्होंने राजा को बताया कि उन्होंने चारों ओर ढूंढ़ कर देख लिया। रैक्व का तो कहीं पता ही नहीं चलता।
राजा ने कहा, ‘‘अरे भई, उसकी तलाश वहां करो जहां ब्राह्मणों की तलाश की जाती है।’’
यूं तो यह बात कहीं नहीं लिखी है कि ब्रह्मविद गाड़ी के नीचे छिप कर बैठे रहते हैं, पर इस बार उन्हें रैक्व को ढूंढ कर निकाल ही लेना था और इसमें वे सफल हुए। कारण, रैक्व के मिले बिना न जानश्रुति पौत्रायण का काम चल सकता था, न हमारी कहानी का। ये जाड़े के दिन थे और रैक्व को खाज हो गई थी। बीमारी यह ऐसा ही कि जिसे हो जाए उसे चैन से बैठने भी नहीं देती और एक बार खुजलाना शुरू कर दिया तो जलन बढ़ती ही जाती है। यह भी ऐसा ही मौका था। जिस समय दूत उसके पास पहुंचा उस समय वह छकड़े के नीचे बैठा अपनी खाज खुजला रहा था।
राजा के दूत ने पूछा, ‘‘क्या आप ही छकड़े वाले रैक्व हैं ?’’
रैक्व ने खुजलाना बंद करके उधर देखा और कहा, ‘‘हां भाई, मैं ही रैक्व हूं।’’
अनुमान किया जाता है कि इसके बाद दूत ने उसे अपना परिचय दिया होगा। परिचय देते हुए उसने सोचा होगा कि उसके इस परिचय का रैक्व पर असर जरूर पड़ेगा, पर या तो इस बीच खुजली तेज हो गई थी जिससे वह झल्ला उठा था, या वह अपने आगे जानश्रुति को कुछ समझता ही नहीं था, इसलिए उसने उसे डांट कर भगा दिया। कहानी थोड़ा लिखना-बहुत-समझना वाली शैली में लिखी गई है अतः परिचय देने और डांट खाने का अनुमान कर लिया गया है। हो सकता है उस व्यक्ति ने रैक्व को अपना परिचय न दिया हो और केवल उसका परिचय जान कर ही लौट गया हो।
जब जानश्रुति को यह बात मालूम हुई तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वह छह सौ गायें, सोने का एक हार और खच्चरियों से जुता हुआ एक रथ ले कर रैक्व के पास आया। यह जमाने की बात है उस जमाने की शिक्षा प्रणाली ऐसी थी कि इसमें गधों को पीट-पीट कर घोड़ा बनाने के स्थान पर घोड़ों को लाद-लाद कर गधा बनाना अधिक श्रेयस्कर समझा जाता था। नतीजा यह था कि घोड़ों का काम भी गधों और खच्चरों को ही निभाना पड़ता था। राजकीय वाहनों में भी अक्सर खच्चर और गधे ही जोते जाते थे।
राजा जो धन ले कर आया था वह किसी को भी अमीर बनाने के लिए काफी था। पर उस समय जब उसे खुजली की दवा ले कर आना चाहिए था वह, बिना सोचे-समझे, इतनी सारी दौलत ले कर आ रहा था। रैक्व गुस्से में आ गया। बोला, ‘‘शूद्र, ले जा अपनी ये गायें और हार और रथ।’’ वह इतने गुस्से में था कि उसने उसे गुस्से का कारण तक नहीं बताया।
जानश्रुति उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने कुछ सोच विचार कर असली कारण भी जान लिया। वह फिर आया। इस बार उसने गायों की संख्या एक हजार कर दी थी। बाकी सामान वही था। जिस गांव में उस समय रैक्व छकड़े के नीचे दुबका पड़ा था उसे भी वह रैक्व को ही देने को तैयार था। उसका एक ही अनुरोध था और यह कि रैक्व उसे उस विद्या का उपदेश अवश्य दे जिसका ज्ञान उसे छोड़कर दूसरों को नहीं था और जिससे दूसरों के पुण्य का लाभ भी उसे ही मिल रहा था। वह उपहारों के साथ में अपनी कन्या को भी लेता आया था जो इतनी सुंदर थी जैसी सुंदरियां केवल कहानियों में ही हुआ करती हैं। रैक्व ने सोचा अब खाने पीने का इंतजाम हो ही गया है, खुजली के लिए यह कन्या भी मिल गई। इस बार नहीं कर दिया तो फिर सारी उम्र इस गाड़ी के नीचे ही कटेगी। जब राजा ने इस बार अनुरोध किया तो उसने उसको झिड़कते हुए कह भी दिया ‘‘शूद्र यह सब जो तू लाया है वह तो ठीक ही है पर मैं यदि तुम्हें उपदेश देने के लिए तैयार हो गया हूं तो धन के लोभ में नहीं, बल्कि इस सुंदर कन्या को देख कर।’’
जिस गांव में वह रैक्व से मिलने आया था वह महावृष देश का रैक्वपर्ण ग्राम था। इसे आज कोई खोजने चले तो कहीं मिलेगा भी नहीं। पर कौन जाने इस कहानी को पढ़ कर किसी ने किसी गांव का यह नाम रख ही लिया हो।
रैक्व ने उपदेश देते हुए कहा, ‘‘वायु ही वह तत्व है जो सबको अपने में मिला लेता है। वही संवर्ग है। आग बुझ कर उसी में लीन होती है। सूर्य वायु में ही अस्त होता है। चंद्रमा अस्त हो कर वायु में ही लीन होता है। जल सूख कर वायु में ही लीन होता है।
भौतिक स्तर पर जो सच है वही आत्मिक स्तर पर भी ठीक है। इस दृष्टि से, प्राण में ही सब कुछ लीन होता है, इसलिए प्राण ही संवर्ग है। हम सोते हैं तो वाणी प्राण में प्रवेश कर जाती है, चक्षु प्राण में लौट जाता है, कान प्राण में समा जाते हैं, मन प्राण में चला जाता है। वही इन सभी को अपने में मिला लेता है। सार यह कि यह वायु या प्राणवायु ही आत्मा है। इससे भिन्न कुछ नहीं है और इसमें बाहर कुछ नहीं है। यही वायु हमारे भीतर है, यही बाहर। सर्वत्र इसी की व्याप्ति है। इसलिए हम वही हैं जो हमारे बाहर है और जो कुछ बाहर दीखता है वही हमारे भीतर है।’’
दान पुण्य से एक खास तरह का तेज पैदा होता है। यह आंखों से तो दिखाई नहीं देता पर इसका प्रभाव सब पर प्रकट होता रहता है। उसका तेज द्युलोक तक फैला हुआ था। उसे स्पर्श करने वाला, उससे स्पर्धा करने वाला, उस तेज से ही भस्म हो सकता था। जैसे चंद्रमा की किरणें दिन में नहीं दिखाई देतीं उसी तरह यह तेज सभी को दिखाई नहीं देता था, पर रात के समय प्रखर दृष्टि रखने वालों को दिखाई दे जाता था। आकाश में यह तेज जिस ऊंचाई तक फैला हुआ था उस ऊंचाई तक आदमी अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकता था। सो रात में आकाश में उड़ते हुए हंसों ने इस तेज को देखा। उनमें से एक हंस ने दूसरे से हंस कर कहा, ‘देखो तो जानश्रुति का तेज आकाश में किस तरह फैला हुआ है। इससे बच कर चलना नहीं तो भस्म हो जाओगे।’’ पर जिस हंस से यह बात कही गई थी उसका सामान्य ज्ञान सलाह देने वाले हंस से अधिक अच्छा था। उसने कहा, ‘‘तुम जानश्रुति पौत्रायण की तारीफ इसलिए कर रहे हो कि तुमको छकड़ेवाले रैक्व के बारे में कुछ पता ही नहीं।’’
अब पहले को जिज्ञासा हुई, छकड़ेवाले रैक्व में ऐसी क्या खास बात है ?
दूसरे हंस ने कहा, ‘‘जुए के खेल में जैसे कृत के पासे के सामने दूसरे सभी पासे ओछे पड़ते हैं और उन पर बदा गया दांव उस खिलाड़ी को मिल जाता है जिसका कृत आ जाता है उसी तरह दूसरे लोग जो भी सत्कर्म करते हैं उसका पुण्य रैक्व के पास पहुंच जाता है। इसकी वजह यह है कि रैक्व जिस विद्या को जानता है उसे कोई नहीं जानता।’’
पौत्रायण को सभी पक्षियों की भाषा न भी मालूम रही हो तो भी हंसों की भाषा तो मालूम थी ही। लगता है उसे अनिद्रा की बीमारी भी थी। हंस अपनी उड़ान रात में ही भरते हैं। वे शुद्ध आत्मा होते हैं इसलिए वे झूठ नहीं बोलते, यह तो सभी जानते हैं। पौत्रायण को उनकी बात पर बहुत भरोसा था। उसने हंसों की बातचीत सुनी तो वह उनकी बात का कायल भी हो गया।
उसके अगले दिन चारणों ने जब उसकी स्तुति आरंभ की तो उसने कहा, ‘‘तुम लोग मेरी स्तुति तो इस तरह कर रहे हो मानो मैं छकड़ेवाला रैक्व होऊं।’’
इस पर उन चारणों को भी रैक्व के विषय में उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा, ‘‘महाराज यह छकड़ेवाला रैक्व कौन है ?’’
राजा ने उन हंसों की बात उन्हें बता दी।
पौत्रायण ने सोचा यदि रैक्व सचमुच इतना तेजस्वी है तो उसका पता लगाना चाहिए और उससे वह विद्या जाननी चाहिए। उसने चारों ओर अपने चर दौड़ाए। रैक्व की तलाश शुरू हुई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस महाप्रतापी की यह महिमा बताई गई है वे गाड़ी के नीचे दुबके बैठे हो सकते हैं, इसलिए रैक्व पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी। एक-एक कर सभी चर लौट आए और उन्होंने राजा को बताया कि उन्होंने चारों ओर ढूंढ़ कर देख लिया। रैक्व का तो कहीं पता ही नहीं चलता।
राजा ने कहा, ‘‘अरे भई, उसकी तलाश वहां करो जहां ब्राह्मणों की तलाश की जाती है।’’
यूं तो यह बात कहीं नहीं लिखी है कि ब्रह्मविद गाड़ी के नीचे छिप कर बैठे रहते हैं, पर इस बार उन्हें रैक्व को ढूंढ कर निकाल ही लेना था और इसमें वे सफल हुए। कारण, रैक्व के मिले बिना न जानश्रुति पौत्रायण का काम चल सकता था, न हमारी कहानी का। ये जाड़े के दिन थे और रैक्व को खाज हो गई थी। बीमारी यह ऐसा ही कि जिसे हो जाए उसे चैन से बैठने भी नहीं देती और एक बार खुजलाना शुरू कर दिया तो जलन बढ़ती ही जाती है। यह भी ऐसा ही मौका था। जिस समय दूत उसके पास पहुंचा उस समय वह छकड़े के नीचे बैठा अपनी खाज खुजला रहा था।
राजा के दूत ने पूछा, ‘‘क्या आप ही छकड़े वाले रैक्व हैं ?’’
रैक्व ने खुजलाना बंद करके उधर देखा और कहा, ‘‘हां भाई, मैं ही रैक्व हूं।’’
अनुमान किया जाता है कि इसके बाद दूत ने उसे अपना परिचय दिया होगा। परिचय देते हुए उसने सोचा होगा कि उसके इस परिचय का रैक्व पर असर जरूर पड़ेगा, पर या तो इस बीच खुजली तेज हो गई थी जिससे वह झल्ला उठा था, या वह अपने आगे जानश्रुति को कुछ समझता ही नहीं था, इसलिए उसने उसे डांट कर भगा दिया। कहानी थोड़ा लिखना-बहुत-समझना वाली शैली में लिखी गई है अतः परिचय देने और डांट खाने का अनुमान कर लिया गया है। हो सकता है उस व्यक्ति ने रैक्व को अपना परिचय न दिया हो और केवल उसका परिचय जान कर ही लौट गया हो।
जब जानश्रुति को यह बात मालूम हुई तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वह छह सौ गायें, सोने का एक हार और खच्चरियों से जुता हुआ एक रथ ले कर रैक्व के पास आया। यह जमाने की बात है उस जमाने की शिक्षा प्रणाली ऐसी थी कि इसमें गधों को पीट-पीट कर घोड़ा बनाने के स्थान पर घोड़ों को लाद-लाद कर गधा बनाना अधिक श्रेयस्कर समझा जाता था। नतीजा यह था कि घोड़ों का काम भी गधों और खच्चरों को ही निभाना पड़ता था। राजकीय वाहनों में भी अक्सर खच्चर और गधे ही जोते जाते थे।
राजा जो धन ले कर आया था वह किसी को भी अमीर बनाने के लिए काफी था। पर उस समय जब उसे खुजली की दवा ले कर आना चाहिए था वह, बिना सोचे-समझे, इतनी सारी दौलत ले कर आ रहा था। रैक्व गुस्से में आ गया। बोला, ‘‘शूद्र, ले जा अपनी ये गायें और हार और रथ।’’ वह इतने गुस्से में था कि उसने उसे गुस्से का कारण तक नहीं बताया।
जानश्रुति उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने कुछ सोच विचार कर असली कारण भी जान लिया। वह फिर आया। इस बार उसने गायों की संख्या एक हजार कर दी थी। बाकी सामान वही था। जिस गांव में उस समय रैक्व छकड़े के नीचे दुबका पड़ा था उसे भी वह रैक्व को ही देने को तैयार था। उसका एक ही अनुरोध था और यह कि रैक्व उसे उस विद्या का उपदेश अवश्य दे जिसका ज्ञान उसे छोड़कर दूसरों को नहीं था और जिससे दूसरों के पुण्य का लाभ भी उसे ही मिल रहा था। वह उपहारों के साथ में अपनी कन्या को भी लेता आया था जो इतनी सुंदर थी जैसी सुंदरियां केवल कहानियों में ही हुआ करती हैं। रैक्व ने सोचा अब खाने पीने का इंतजाम हो ही गया है, खुजली के लिए यह कन्या भी मिल गई। इस बार नहीं कर दिया तो फिर सारी उम्र इस गाड़ी के नीचे ही कटेगी। जब राजा ने इस बार अनुरोध किया तो उसने उसको झिड़कते हुए कह भी दिया ‘‘शूद्र यह सब जो तू लाया है वह तो ठीक ही है पर मैं यदि तुम्हें उपदेश देने के लिए तैयार हो गया हूं तो धन के लोभ में नहीं, बल्कि इस सुंदर कन्या को देख कर।’’
जिस गांव में वह रैक्व से मिलने आया था वह महावृष देश का रैक्वपर्ण ग्राम था। इसे आज कोई खोजने चले तो कहीं मिलेगा भी नहीं। पर कौन जाने इस कहानी को पढ़ कर किसी ने किसी गांव का यह नाम रख ही लिया हो।
रैक्व ने उपदेश देते हुए कहा, ‘‘वायु ही वह तत्व है जो सबको अपने में मिला लेता है। वही संवर्ग है। आग बुझ कर उसी में लीन होती है। सूर्य वायु में ही अस्त होता है। चंद्रमा अस्त हो कर वायु में ही लीन होता है। जल सूख कर वायु में ही लीन होता है।
भौतिक स्तर पर जो सच है वही आत्मिक स्तर पर भी ठीक है। इस दृष्टि से, प्राण में ही सब कुछ लीन होता है, इसलिए प्राण ही संवर्ग है। हम सोते हैं तो वाणी प्राण में प्रवेश कर जाती है, चक्षु प्राण में लौट जाता है, कान प्राण में समा जाते हैं, मन प्राण में चला जाता है। वही इन सभी को अपने में मिला लेता है। सार यह कि यह वायु या प्राणवायु ही आत्मा है। इससे भिन्न कुछ नहीं है और इसमें बाहर कुछ नहीं है। यही वायु हमारे भीतर है, यही बाहर। सर्वत्र इसी की व्याप्ति है। इसलिए हम वही हैं जो हमारे बाहर है और जो कुछ बाहर दीखता है वही हमारे भीतर है।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book