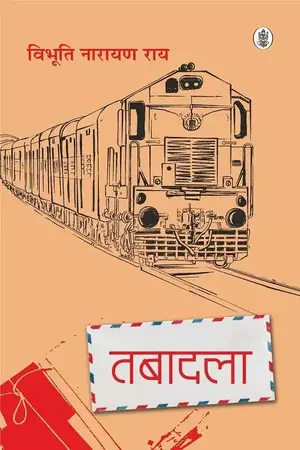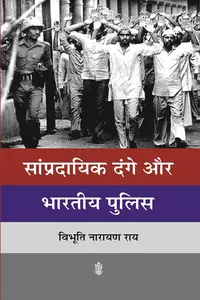|
उपन्यास >> तबादला तबादलाविभूति नारायण राय
|
181 पाठक हैं |
|||||||
"बदली हुई नौकरी, बदलती हुई व्यवस्था : भारतीय नौकरशाही की कड़वी सच्चाई"
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ती मौजूदगी और कारपोरेट दुनिया में कार्य-संस्कृति पर लगातार एक नैतिक मूल्य के रुप में जोर दिए जाने के बावजूद भारतीय मध्यवर्ग की पहली पसन्द आज भी सरकारी नौकरी ही है, तो उसका सम्बन्ध, उस आनन्द से ही है जो गैर-जिम्मेदारी, काहिली, अकुंठ स्वार्थ और भ्रष्ठाचार से मिलता है; और हमारे स्वाधीन पचास सालों में सरकारी नौकरी इन सब ‘गुणों’ का पर्याय बनकर उभरी है। इन्हीं के चलते तबादला-उद्योग वजूद में आया जो आज दफ्तरों से लेकर राजनेताओं के बंगलों तक, शायद बाकी कई उद्योगों से ज्यादा, फल-फूल रहा है।
इस उद्योग के जिन बारीक डिटेल्स को हम बिना इसके भीतर उतरे, बिना इसका हिस्सेदार बने, नहीं जान सकते, उन्हीं को उपन्यास इतने तीखे और मारक व्यंग्य के सामने रखता है कि हमें उस हताशा को लेकर नए सिरे से चिन्ता होने लगती है जो भारतीय नौकरशाही ने पिछले पचास सालों में आम जनता को दी है। इस उपन्यास का वाचक व्यंग्य के उस ठंडे कोने में जा पहुँचा है जहाँ ‘कोई उम्मीदबर नहीं आती’। उपन्यास पढ़कर हम सचमुच यह सोचने पर बाध्य हो जाते हैं कि अगर यह हताशा वास्तव में हमारे इतने भीतर तक उतर चुकी है तो फिर रास्ता है किधर !
बड़े साहब की बदली को सिर्फ एक दिन हुआ था। बटुकचन्द्र को दफ्तर के लोग पहले से जानते थे लेकिन उन्होंने कोई जोखिम लेना मुनासिब नहीं समझा। आज दस बजे तक सारे बाबू तफ्तर में आ गए थे। आने पर उन्हें कमरे खुले भी मिले। आकर वह फौरन चाय की दुकानों पर नहीं गए बल्कि उन्होंने अपने सामने रखी फाइलों में कुछ लिखा भी। बटुकचन्द्र भी सवा दस बजे आ गए। उन्होंने भी कुछ फाइलों पर दस्तखत किए। घंटे-डेढ़ घंटे दफ्तर में जो कुछ हुआ, उसे देखकर कुछ पुराने दलाल यह सोचकर कि वे किसी दूसरे दफ्तर में चले आए हैं, बाहर भाग गए।
लाल फीते से फाइल बँधते ही मान लिया जाता था कि उसमें बन्द कागजों के आराम में अब अगली दो-तीन पीड़ियों तक कोई खलल नहीं डालेगा। इसी से भाषा को एक नया शब्द मिला-लाल फीताशाही। हमारे देश में बाज मुख्यमन्त्रियों को यह शब्द पसन्द नहीं आया, इसलिए उन्होंने लाल की जगह हरे, पीले, गुलाबी जैसे रंगों के पत्ते इस्तेमाल करने के हुक्म दे दिए। इस तरह लाल फीताशाही खत्म हो गई और कागज दूसरे रंगों फीतों के नीचे दफन होने लगे।
हर अफसर नौकरी शुरु करते ही जान जाता है कि उसे और कुछ करना हो, न हो, पर दस्तखत बहुत करने होंगे। इसलिए वह अपने हस्ताक्षरों का एक लघु संस्करण ईजाद करता है, जिसे चिड़िया कहते हैं।...कमीशन की खुशबू बिखेरनेवाली फाइल पर बैठी चिड़िया चहकती नजर आती है और सूखे कागजों पर बैठी हुई मरियल। हमारे देश में, जिस तरह के विषयों पर शोध हो रहा है, उसे देखते हुए इस बात की पूरी सम्भावना है कि विश्वविद्यालयों में किसी दिन इस महत्त्वपूर्ण विषय पर भी काम होगा।
इस उद्योग के जिन बारीक डिटेल्स को हम बिना इसके भीतर उतरे, बिना इसका हिस्सेदार बने, नहीं जान सकते, उन्हीं को उपन्यास इतने तीखे और मारक व्यंग्य के सामने रखता है कि हमें उस हताशा को लेकर नए सिरे से चिन्ता होने लगती है जो भारतीय नौकरशाही ने पिछले पचास सालों में आम जनता को दी है। इस उपन्यास का वाचक व्यंग्य के उस ठंडे कोने में जा पहुँचा है जहाँ ‘कोई उम्मीदबर नहीं आती’। उपन्यास पढ़कर हम सचमुच यह सोचने पर बाध्य हो जाते हैं कि अगर यह हताशा वास्तव में हमारे इतने भीतर तक उतर चुकी है तो फिर रास्ता है किधर !
बड़े साहब की बदली को सिर्फ एक दिन हुआ था। बटुकचन्द्र को दफ्तर के लोग पहले से जानते थे लेकिन उन्होंने कोई जोखिम लेना मुनासिब नहीं समझा। आज दस बजे तक सारे बाबू तफ्तर में आ गए थे। आने पर उन्हें कमरे खुले भी मिले। आकर वह फौरन चाय की दुकानों पर नहीं गए बल्कि उन्होंने अपने सामने रखी फाइलों में कुछ लिखा भी। बटुकचन्द्र भी सवा दस बजे आ गए। उन्होंने भी कुछ फाइलों पर दस्तखत किए। घंटे-डेढ़ घंटे दफ्तर में जो कुछ हुआ, उसे देखकर कुछ पुराने दलाल यह सोचकर कि वे किसी दूसरे दफ्तर में चले आए हैं, बाहर भाग गए।
लाल फीते से फाइल बँधते ही मान लिया जाता था कि उसमें बन्द कागजों के आराम में अब अगली दो-तीन पीड़ियों तक कोई खलल नहीं डालेगा। इसी से भाषा को एक नया शब्द मिला-लाल फीताशाही। हमारे देश में बाज मुख्यमन्त्रियों को यह शब्द पसन्द नहीं आया, इसलिए उन्होंने लाल की जगह हरे, पीले, गुलाबी जैसे रंगों के पत्ते इस्तेमाल करने के हुक्म दे दिए। इस तरह लाल फीताशाही खत्म हो गई और कागज दूसरे रंगों फीतों के नीचे दफन होने लगे।
हर अफसर नौकरी शुरु करते ही जान जाता है कि उसे और कुछ करना हो, न हो, पर दस्तखत बहुत करने होंगे। इसलिए वह अपने हस्ताक्षरों का एक लघु संस्करण ईजाद करता है, जिसे चिड़िया कहते हैं।...कमीशन की खुशबू बिखेरनेवाली फाइल पर बैठी चिड़िया चहकती नजर आती है और सूखे कागजों पर बैठी हुई मरियल। हमारे देश में, जिस तरह के विषयों पर शोध हो रहा है, उसे देखते हुए इस बात की पूरी सम्भावना है कि विश्वविद्यालयों में किसी दिन इस महत्त्वपूर्ण विषय पर भी काम होगा।
-इसी पुस्तक से
एक
सर पर कुम्भ और तबादला ! अगर मुहावरे की भाषा में कहा जाए तो श्री कमलाकान्त वर्मा, अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए यह स्थिति किसी वज्राघात से कम नहीं थी। अक्तूबर खत्म हो रहा था और कुम्भ का काम धीरे-धीरे जोर पकड़ने लगा था। ज्यादातर कामों के टेंडर हो चुके थे। कुछ काम अवार्ड हो चुके थे, कुछ पर निर्णय की प्रक्रिया अपने अन्तिम चरण में थी। मेला क्षेत्र में सड़के आकार लेने लगी थीं, और पुलों के लिए पीपे नदी के किनारे पहुँचने लगे थे। बल्लियाँ, शामियाने, चेकर प्लेटें ढेर-के-ढेर गंगा-यमुना के तट पर पड़े थे। जीप से मेला क्षेत्र में जब भी कमलाकान्त निकलते तो लगभग हर बार बन्धे पर कहीं गाड़ी रुकवाकर क्षेत्र में फैले इन सारे सामानों पर देर तक सन्तुष्ट नजर डालते। इनसे टकराकर आती हुई हवा को वे गहरी साँसें खींचकर अपने फेंफड़ों में भरते। लगता जैसे कि सरकारी नोट छापने की मशीनों से टकराकर आ रही हो यह हवा। शीतल और स्फूर्ति देनेवाली।
ऐसे समय में तबादला ! जितना कुछ खर्च करके वे यहाँ आए हैं, अभी तो दसवाँ हिस्सा भी नहीं निकला। बचत की तो बात ही क्या की जाए। इसलिए कमलाकान्त वर्मा, जिन्हें दफ्तर में सब लोग बड़े साहब कहते हैं, हतप्रभ हैं और दफ्तर का कमरा बन्द कर अपने विशेष मातहतों के साथ उस आदेश पर विचार-विमर्श कर रहे हैं जिसे अभी-अभी मुख्यालय का एक चपरासी थमा गया है।
कमरे में वर्मा साहब के अलावा चार लोग और थे। ये चार लोग अलग-अलग कामों से वहाँ मौजूद थे। एक कारण ऐसा था जो चारों की उपस्थित के पीछे था दफ्तर में सत्ता-परिवर्तन हो रहा था। ये चारों सत्ता पक्ष के लोग थे। नौकरशाही में भी राजनीति की तरह सत्ता परिवर्तित होते ही मुँह फेरने की परम्परा शुरू हो गई थी, पर ये लोग कुछ हयादार लगते थे, जो तबादले का आदेश आने के बाद भी मन्त्रणा के लिए उपलब्ध थे। या यह भी हो सकता है कि छोटे-मोटे बनाना रिपब्लिकों की तरह यहाँ भी अभी सब कुछ अनिश्चित था। तख्तापलट हो भी सकता है और यह भी हो सकता है कि शाहे-वक्त दुश्मन के हाथी-घोड़ों को रौंदता हुआ वापस गढ़ पर काबिज हो जाए। वैसे भी इस प्रदेश में नौकरशाही के तबादलों के हुक्म नीलाम होते थे। दिन में चार बार भी उनमें परिवर्तन हो सकता था। जो भी कारण हो ये चारों लोग तबादले का आदेश आने के बाद भी वहाँ थे और आदेश को बार-बार उलट-पुलटकर पढ़ रहे थे, फुसफुसाकर बातें कर रहे थे और बड़े साहब को अपनी बहुमूल्य राय दे रहे थे।
वर्मा साहब के बाईं तरफ थे रिजवानुल हक जो इस दफ्तर में सहायक अभियन्ता थे। पचास के पेटे में पहुंचा उनका शरीर बीमारी और दुर्घटनाओं के कारण लगभग ढल चुका था। माथे के ऊपर आधी सफाचट चाँद के कारण उनका पूरा व्यक्तित्व काफी गम्भीर किस्म का लगता था। वे कम बोलते थे और बिना माँगे कभी राय नहीं देते थे। दफ्तर में कोई भी बड़ा साहब आ जाए उनको इसी आदत के कारण अपना राजदार बना लेता था। लोगों को याद नहीं पड़ता था कि कभी किसी अधिशासी अभियन्ता से उनकी नहीं पटी हो।
जब कमलाकान्त वर्मा यहाँ आए तो कुछ दिनों तक उनसे भड़कते रहे। कारण सिर्फ यह था कि वे उनके पूर्वाधिकारी के करीब थे और पिछली बार जब वर्मा इसी तरह का आदेश कराकर लखनऊ से रवाना हुए तो उनके पूर्वाधिकारी ने अपने बँगले पर जो आपात बैठक बुलाई थी उसमें वे भी शरीक हुए थे। दफ्तर में कुछ दिनों तक हक साहब को बेचैन देखा गया। उनके विरोधियों ने चटखारे ले-लेकर वास्तविक, अर्द्ध वास्तविक और काल्पनिक खबरें प्रसारित कीं कि किस तरह हक साहब को बड़े साहब के कमरे में घुसने के पहले तीन घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती है या कि उनके पास अब कोई महत्त्वपूर्ण काम नहीं है या कि जल्दी ही बड़े साहब उन्हें डिजाइन सेक्शन में शंट कराने वाले हैं।
हक साहब इन सारी चर्चाओं से विचलित नहीं हुए। दफ्तर के अनुभवी बाबुओं की तरह उन्हें भी पता था कि यह तो अस्थायी दौर है। यह हर बार सत्ता परिवर्तन के साथ आता है, फिर कुछ महीनों में ठीक हो जाता है। इस बार भी यही हुआ। कभी ईद पड़ी, कभी बकरीद। हक साहब की बेगम अच्छा मुर्गा पकाती थीं और वर्मा साहब की पत्नी खाने की शौकीन थीं। पहली ईद पर हक बड़े साहब के बेरुखे मुबारकबाद के बावजूद दोहरे होते हुए बोले, ‘‘सर, मेरी फैमिली की बड़ी इच्छा थी कि मैडम और बच्चे हमारे गरीबखाने पर तशरीफ लाते पर आप इतने बिजी रहते हैं कि अर्ज करने की हिम्मत नहीं पड़ी और मैं खुद ही हाजिर हुआ हूँ। बेगम ने अपने हाथ से मुर्गा पकाया है। उम्मीद है बच्चों को पसन्द आएगा।’’
मुर्गा बच्चों को खूब पसन्द आया पर वर्मा साहब की फाँस अभी दूर नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों हक साहब की बेगम साहिबा किसी न किसी मौके पर मुर्गे या बकरे की कोई लजीज डिश बनाकर भेजती रहीं।
विरोधी खेमे का चपरासी बड़े साहब के घर पर तैनात था। उससे बात खुली तो यह खेमा चौकन्ना हुआ।
एक शाम जब दो टिफिन कैरियरों में भरकर मटन कोरमा, चिकन मुगलाई, मटन यखनी और सींक कबाब जैसी चीजों के साथ जानीवाकर ब्लैक लेबल की बोतल इस आग्रह के साथ पहुंची कि ‘सर मेरा साला कल सऊदी अरब से आया है। वही एयरपोर्ट से मेरे लिए ड्यूटी फ्री स्काच ले आया। अब मैंने तो छोड़ रखी है। साला ठहरा नमाजी, हाथ नहीं लगाता। बेगम ने कहा बड़े साहब इसकी कद्र जानते हैं, उन्हें यह तोहफा दे आओ। साथ में थोड़ा सा नान वेजिटेरिनयन बच्चों के लिए लेते जाओ। पता नहीं कैसा बना है। मेम साहब ने कभी राय नहीं दी, ‘‘विरोधी कैम्प सक्रिय हो गया। गुप्तचर छोड़े गए और जो सूचना वे लेकर आए उससे इस कैम्प की बाँछें खिल गईं।
दूसरे दिन बड़े साहब के कमरे में स्टाफ मीटिंग के दौरान जब चाय का मध्यान्तर हुआ तो हल्की-फुल्की बातों के दौरान सहायक अभियन्ता गुप्ता ने हक से ऐसे ही अनायास पूछ लिया, ‘‘भाभी को कब ला रहे हैं हक साहब ? कब तक मातादीन के हाथ का खाना खाएंगे।?’’
हक साहब ने चौंककर देखा। वे बोलते कम थे पर उनका दिमाग बड़ी तेज हरकत करता था। स्पष्ट था कि बड़े साहब को विरोधी खेमा यह बताने की कोशिश कर रहा है कि पिछले दो महीने से उनकी पत्नी अपने मायके बाराबंकी गई हुई हैं और वे करीम ढाबे से मुर्गा बनवाकर अपनी बेगम के नाम पर बड़े साहब को खिला रहे थे।
बड़े साहब ने चाय का प्याला नीचे रख दिया और हल्के से चश्मा हाथ में लेकर उसे रूमाल से पोंछने लगे।
‘‘बेगम तो बाराबंकी और यहाँ के बीच चक्कर लगाती रहती हैं। दरअसल, सर, जब से फादर-इन-ला की तबीयत खराब हुई है उन्हें दो जगह के इन्तजाम देखने पड़ रहे थे। एक ही भाई है उनका जो सऊदी अरब में है। जमींदारी है-छोड़ी भी नहीं जा सकती। बेगम को ही देखनी पड़ रही है। कल साला उन्हें लेकर आया था। आज फिर वापस गए हैं वे लोग।’’
विरोधी खेमे के लोग इस तरह मुस्कुराए कि किसी और को मुस्कान दिखाई दे न दे, बड़े साहब को जरूर दिखाई दे जाए।
अपने देश में पिछले कुछ सालों में और कोई तरक्की हुई हो या नहीं पर इलेक्टॉनिक एक्सचेंजों की बहार जरूर आ गई है। मोहल्ले-मोहल्ले में खुले पी.सी.ओ.में एक बार बाराबंकी के लिए सक्रिय हुआ और देर रात तक बेगम हक शहर में हाजिर हो गईं। विरोधी खेमा दूसरे दिन हतप्रभ रह गया, जब उसे पता चला कि मेम साहब की बीमारी की खबर, जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, सुनकर बेगम साहिबा बड़े साहब के घर अगले दिन दोपहर हालचाल पूछती देखी गईं। साथ में पिछले दिन से बड़ा टिफिन कैरियर था।
बाद में जैसा कि पिछले कई मौकों पर हुआ था और दफ्तर के अनुभवी बाबू पहले से जानते थे, वैसा ही हुआ। वे बड़े साहब की अन्तरंग टीम के सदस्य बन गए और उसी हैसियत से आज की मन्त्रणा में शरीक थे।
कमरे में वर्मा साहब के दाहिनी तरफ बैठे हुए व्यक्ति की उपस्थिति का कारण बड़ा दिलचस्प था। छोटे-छोटे बाल, गैंडे जैसी गर्दन और टूटे हुए कानवाले इन सज्जन को किसी अखाड़े में होना चाहिए था। वे दफ्तर में थे पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके जीवन का मूलमन्त्र था कि पूरा जीवन ही अखाड़ा है। वे कभी भी कहीं भी कुश्ती लड़ने के लिए तैयार रहते थे। चूँकि अपने जागृत समय का बड़ा हिस्सा वे दफ्तर में बिताते थे इसलिए मौजूदा जीवन की अधिकांश कुश्तियां भी वे यहीं लड़ते थे। अक्सर उनके साथ बातचीत करने वाले को उनकी कुश्ती कला से परिचित होने का अवसर मिलता था। धोबिया पाट उनका प्रिय दाँव था और दफ्तर के बरामदों में अगर कोई कर्मचारी, ठेकेदार या मुलाकाती लँगड़ाता हुआ दिखाई दे जाता तो बिना बताए लोग मान लेते कि वह व्यक्ति इनसे कुछ गम्भीर विचार-विमर्श करके जा रहा है।
ध्रुवलाल यादव नामक ये सज्जन जूनियर इंजीनियर थे और डॉ. रघुबीर जैसे उत्साही हिन्दी-प्रेमियों की मेहनत को धता बताते हुए लोग उन्हें अवर अभियन्ता न कहकर जे.ई. कहते थे। वे जे.ई. थे इसलिए जब तक बोलते या लिखते नहीं थे, लोग मानकर चलते थे कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जरूर हासिल किया होगा। जैसे ही उनके श्रीमुख से कोई वाक्य निकलता या वे कागज पर अपने पेशे से संबंधित कोई चीज लिखते, सामनेवाला मान लेता कि वे भी उन फैक्टरियों से निकला हुआ माल थे जिन्हें हमारे शिक्षाविद् स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या पालीटेक्नीक के नाम से पुकारते थे और जो धड़ाधड़ साल-दर-साल हजारों लाखों की तादाद में ध्रुवलाल जैसे होनहार निकालते रहते हैं। उन्होंने पालीटेक्नीक में पढ़ाई के अतिरिक्त प्रयुक्त होनेवाले दो तरीकों में से एक का प्रयोग करके डिप्लोमा हासिल किया था। उनके द्वारा प्रयुक्त तरीका विभाग में भी बड़ा काम आता है, यह उन्हें नौकरी शुरू करने पर ही पता चला।
जे.ई.ध्रुवलाल यादव के सामने जीवन की प्राथमिकताएँ शुरू से ही बड़ी स्पष्ट थीं। उनके बाप मझोले दर्जे के काश्तकार थे और लगभग बीस भैंस-गायों की सेवा-सुश्रुवा करके अपने परिवार को औसत भारतीय किसान की जिन्दगी से बेहतर जीवन प्रदान किए हुए थे। लेकिन ध्रुवलाल अपने परिवेश के मुकाबले ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। टखने-टखने तक गोबर में डूबकर गाय-भैसों की सेवा करना और शाम को कान पर हाथ रखकर बिरहा गाना-सिर्फ इन्हीं दो कामों तक वे अपनी जिन्दगी सीमित नहीं रख सकते थे। लिहाजा उन्होंने पढ़ने का फैसला किया। बाप के बहुत बच्चे थे। जमाना भी बदल रहा था। अपने लिए अब ‘करिया अच्छर भैंस बराबर’ सुनना बाप को खलने लगा था। इसलिए एक लड़के का पढ़ाई की तरफ रुझान उसके लिए खुशी की बात थी। उसने औपचारिक रूप से ससुरी महँगाई का जिक्र जरूर किया पर ध्रुवलाल को शहर भेज दिया।
बचपन से ही घी-दूध का सुख होने तथा बाप के प्रिय मुहावरे के अनुसार जूता मारकर सुबह-सुबह अखाड़े में ठेले जाने के कारण ध्रुवलाल एक अदद कसरती बदन के मालिक थे। उनका कद छह फुट से कुछ ऊपर था, दोनों तरफ से कान टूटे हुए थे, रंग गन्दुम और स्वर लट्ठमार हद तक उजड्ड था। यही सारी चीजें उनकी पूँजी थीं। सबसे पहले यह पूँजी पालीटेक्नीक में काम आई।
पालीटेक्नीक में पहुंचने के पहले दो-तीन हफ्ते में ही यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में छपी पाठ्य-पुस्तकें उनकी लिए ग्रीक और लैटिन के महाकाव्यों की तरह थीं।
ध्रुवलाल यादव के ईमानदार मन ने उन्हें सलाह दी कि भाग चल प्यारे ! कहाँ फँस गया ! जीवन इन किताबों से परे ज्यादा सुखद है। दर्जा आठ में किसी कवि ने, जिसका नाम स्वाभाविक था कि वे भूल गए थे, सही ही लिखा था कि अहा ! ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे। पर आगे काशी फल कूष्मांड के साथ-साथ भूसा, गोबर और बाप के जूते का ऐसा त्रिकोण फ्लैश बैक की तरह सामने आता कि वे तो वे उनका ईमानदार मन भी काँप जाता। उन्होंने अपने मन की अनसुनी कर दी और सफलता के गुर दूसरी जगह तलाशने शुरू कर दिए।
भारतीय समाज में बिरादरी बहुत बड़ा सम्बल है। ध्रुवलाल के काम भी यही सम्बल आया। पहले रैगिंग के समय भी यह सम्बल उनके साथ था। रैगिंग में तो उनका डील-डौल और टूटे हुए कान भी निपट लेते पर पढ़ाई में मामला कुछ दूसरा था। उनके बिरादरी के सीनियरों ने बताया कि सूबे के दूसरे पालीटेक्नीकों की तरह इस पालीटेक्नीक में भी सफलता के लिए पढ़ाई के अलावा दो रास्ते थे। पढ़ाई तो निरीह छात्र करते थे। ध्रुवलाल सरीखों को तो शेष दो रास्तों में से एक चुनना था।
पहला रास्ता था बाहुबल का और दूसरा था धनबल का। बाहुबली छात्र कट्टा या चाकू मेज पर रखते और आराम से किताबें खोलकर नकल करते। इन बाहुबली छात्रों की प्रतिभा सत्र के प्रारम्भ में ही पहचान ली जाती और अध्यापकों का कोई न कोई गुट उनके सिर पर वरद-हस्त रख देता। बाहुबली से यह गुट साल-भर अपने विरोधी अध्यापकों को पिटवाता या गाली दिलवाता और इत्महान में इन्हें पर्चा आउट करने से लेकर छोटी-छोटी पुर्जियों पर उतर लिखकर पहुँचाने तक का काम करता।
दूसरा रास्ता था धनबल का। जिस समय ध्रुवलाल पालीटेक्नीक में पहुंचे भारतीय समाज में बहुत कुछ बदल रहा था। शिक्षा की दुनिया बदल रही थी और उससे जुड़े गुरु बदल रहे थे। अब गुरु राजपुत्रों को दौड़ जिताने के लिए निर्धन शिष्यों के अँगूठे नहीं कटवाते थे। वे धनिक पुत्रों से वाजिब फीस लेकर उन्हें दौड़ शुरू होने से पहले ही आगे कर देते थे। प्रधानाध्यापकों और कॉलेजों के मैनेजरों ने नकल को एक व्यवस्थित रोगजार का रूप दे दिया था। हर चीज के रेट निर्धारित हो गए थे। यदि अपने तयशुदा कक्ष में नकल करनी थी तो उसकी एक कीमत थी, किसी अलग कमरे में बैठकर सहायक की मदद से उत्तर पुस्तिका लिखनी थी तो उसकी दूसरी कीमत थी, किसी दूसरे को बैठाकर उससे उत्तर पुस्तिका लिखवाने की कीमत अलग थी और अगर कोई छात्र चाहते कि विषय का अध्यापक ही उसके पास खड़ा होकर इमला दे तो इसकी फीस सबसे भिन्न थी।
ध्रुवलाल ने पहला रास्ता चुना। वे एक-एक कर सारी कक्षाएँ पास करते गए। यह रास्ता परीक्षा पास करने के अलावा नौकरी में भी उनके काम आया। प्रारम्भ में जब वे इस दफ्तर में आए उनकी छवि पहले ही यहाँ पहुंच चुकी थी। अपने सुगठित शरीर और उज़ड्ड जुबान के साथ वे एक ऐंटी इस्टैब्लिसमेंट छवि लिये दफ्तर में घुसे। नियुक्ति पत्र के मुताबिक जिस समय उन्हें वहाँ होना चाहिए था उससे वे सिर्फ पाँच महीने लेट थे। हुआ यह कि सरकारी नौकरी मिलने के पहले ही उन्हें कहीं विदेश में भी नौकरी दिलाने का भरोसा किसी एजेंट ने दिया था। अत: इस नौकरी का नियुक्ति-पत्र जेब में रखे वे विदेशी नौकरी के लिए दौड़ते रहे और अन्त में निराश होकर पाँच महीने बाद ज्वाइन करने इस दफ्तर में पहुँचे। पहुँचते ही उनके और बड़े बाबू के बीच में बड़ी संवैधानिक किस्म की बहस छिड़ गई। बड़े बाबू के मुताबिक कोई भी नियुक्ति-पत्र कुछ खास समय तक ही वैध रहता है। कम से कम पांच महीने तक तो नहीं ही रहता। उनकी राय में ध्रुवलाल यादव को फिर से जाकर अपने नियुक्ति-पत्र का नवीनीकरण कराना चाहिए था। इसके विपरीत ध्रुवलाल का मानना था कि एक बार नियुक्ति-पत्र मिलने के बाद रिटायरमेंट की उम्र तक प्रभावी रहता है। उन्होंने बड़े बाबू को चुनौती भी दी कि वे एक भी नियम ऐसा दिखा दें जिसके मुताबिक कोई नियुक्ति-पत्र पाँच महीने बाद रद्द हो जाता है। बड़े बाबू कोई भी ऐसा नियम नहीं दिखा पाये। फिर भी बड़े बाबू को धर्मसंकट से उबारने के लिए उन्होंने मीठे स्वर में आग्रह किया कि उन्हें पाँच महीने पहले की निर्धारित तारीख में ही ज्वाइन करा दिया जाए।
बड़े बाबू जो दप्तर के दूसरे बाबूओं की तरह उन्हें उनके सुगठित शरीर और मुंह में ठूँसे हुए पान के कारण ‘महिमा बरनि न जाए’ वाले भाव से निहार रहे थे, उनके इस आग्रह पर एकदम से बड़े बाबू बन गए। उन्होंने अपने तीस साल की बाबूगिरी का निचोड़ फाइनेंसियल हैंडबुक के फलाँ पेज और अलाँ पैरे तथा गवर्नमेंट सर्वेंट्स कांडक्ट रूल्स के पेज नं. इतने से इतने तक के उद्धरण के रूप में देना शुरू कर दिया जिसे ध्रुवलाल काफी अनिच्छा और अधैर्य के साथ झेलते रहे। इसीलिए पब्लिक सेक्टर इस मुल्क में असफल हो रहा है-उन्होंने निराशा से सोचा और हवा में मुँह उठाकर किसी काल्पनिक व्यक्ति की माँ-बहन के साथ अपने शारीरिक सम्बन्ध कायम करने लगे। बड़े बाबू अगर काफी मोटी चमड़ी के न होते तो इन सम्बोधनों को अपने लिए ही समझ लेते पर वे निर्विकार भाव से किसी फाइल में डूब गए। दूसरे बाबुओं ने जरूर आँखें मटकाईं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अपने उद्गारों से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि श्री ध्रुवलाल जिन स्त्रियों के सम्मान में कसीदे पढ़ रहे थे वे बड़े बाबू की ही पत्नी और बेटियाँ थी।
बड़े बाबू ने भारतीय नौकरशाही का मूल मन्त्र पकड़ा। जब कोई फैसला न करना हो तो फौरन फाइल पर लिखो-बात करें। यहाँ उनके नीचे कोई ऐसा नहीं था जिसके पास ‘प्लीज स्पीक’ लिखकर वे फाइल भेज सकते थे और यमदूत की तरह ध्रुवलाल सामने खड़े थे इसलिए वे भुनभुनाते हुए स्वयं ही उनका नियुक्ति पत्र लेकर उठ खड़े हुए और बड़े साहब के कमरे की तरफ बात करने के लिए बढ़ गए और दो-तीन घंटे तक नहीं लौटे।
इन दो-तीन घंटों का बड़े साहब के विरोधियों ने जमकर सदुपयोग किया। दूसरे दफ्तरों की तरह इस दफ्तर में भी काम होता हो या नहीं, राजनीति खूब होती थी। कौटिल्य ने सहस्रों वर्षों पूर्व राजनीति और गुप्तचरी का सम्बन्ध परिभाषित कर दिया था और यह दफ्तर पूरी श्रद्धा के साथ उस पर विश्वास करता था। सरकारी गुप्तचर एजेंसियों की तरह यहाँ गोपनीय सूचनाएँ अखबारों की करतनों से नहीं उपजती थीं बल्कि इन्हें हासिल करने के लिए मेहनत की जाती थी, इसलिए अक्सर इनमें कुछ दम भी होता था। ध्रुवलाल यादव का कमरे में प्रवेश, बड़े बाबू के साथ उनके नाटकीय संवाद और बाबुओं की प्रतिक्रिया के बीच अचानक जायसवाल नामक ठेकेदार क्यों ? बाबुओं की सेवा के लिए लाया गया मगही पान का आधे से ज्यादा भाग खोखा तिवारी बाबू की मेज पर छोड़कर कमरे से गायब हो गया, इसका पता करने के लिए अशोक कुमार शुक्ला सहायक अभियन्ता अर्थात् ए.ई.के कमरे में चलना पड़ेगा जो इस कमरे से तीन कमरे दूर था और जिसमें चौरसिया नामक एक अन्य ए.ई.भी बैठते थे और जो इस समय किसी साइट पर गए हुए थे। उनके न होने से ही ध्रुवलाल वहाँ निमन्त्रित किए गए थे। अगर वे होते तो यह गोष्ठी कहीं और होती क्योंकि उनके बारे में शुक्ला का मानना था कि वे बड़े साहब के गुप्तचर थे और उन्हें इस कमरे में बिठाया ही इसलिए गया था कि वे शुक्ला एंड कम्पनी पर निगरानी रख सकें।
इस कमरे में ध्रुवलाल यादव की दफ्तरी दीक्षा शुरू हुई।
कमरे में दो मेजें थीं। दो मेजें इसलिए थीं कि सिर्फ दो ही मेजें उसमें आ सकती थीं। दोनों मेजों के पीछे एक-एक कुर्सी थी। एक कुर्सी का एक हत्था उखड़ा हुआ था और पीछे के ताँत भी जगह-जगह से टूटे हुए थे, उस पर शुक्ला बैठे हुए थे। दूसरी कुर्सी घूमनेवाली थी और उस पर न सिर्फ मैली सी एक गद्दी थी बल्कि पीछे एक लिहाफ भी था जो शुरू में जरूर सफेद रहा होगा पर अब बदरंग हो चुका था। कुर्सियों की यह दशा दफ्तर में बड़े साहब से निकटता का पैमाना था।
दोनों मेजों के सामने दो कुर्सियाँ थीं। चार में से कोई कुर्सी साबुत नहीं थी। किसी के पीछे के ताँत टूटे थे और किसी के नीचे के, किसी हत्था हिल रहा था तो किसी के पांव डगमग कर रहे थे। मेजों पर बेतरतीब फाइल कवर कागज पेपरवेट और पान के खोखे फैले हुए थे। पूरे कमरे में सिगरेट के टुकड़े और राख बिखरी हुई थी और कमरे के हर कोने में दीवारें पान की पीक से अमूर्त चित्रकला का नमूना पेश कर रही थीं। दफ्तर में बड़े साहब के कमरे को छोड़कर सभी कमरों की ऐसी ही हालत थी और इस कमरे में भी दूसरे कमरों की तरह सरकारी काम के अलावा सब कुछ होता था।
इसी कमरे में ध्रुवलाल यादव नौकरशाही में दीक्षित हुए। उन्हें चौरसिया ठेकेदार कनखियों से इशारा करते हुए यहाँ तक ले आया था।
कमरे में शुक्ला नामक सहायक अभियन्ता या ए.ई. के अलावा दो जे.ई. और एक बाबू पहले से थे। छोटे से कमरे में उन्होंने सामने पड़ी कुर्सियों का रुख इस तरह मोड़ लिया था कि पहली बार घुसने पर किसी गोलमेज सम्मेलन का सा माहौल लगता था। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, ध्रुवलाल ने चौथी खाली पड़ी कुर्सी पर कब्जा कर लिया। जायसवाल ने चारों तरफ इस प्रकार देखा मानो उसकी दृष्टि से वहां कोई कुर्सी उत्पन्न हो जाएगी। अभी उसकी हैसियत ऐसी नहीं थी कि शुक्ला उसे चौरसिया की कुर्सी पर बैठने को कहते इसलिए थोड़ी देर इधर-उधर देखकर वह ‘अभी पान लेकर होता हूँ, जैसा कोई वाक्य बुदबुदाकर अदृश्य हो गया।
‘‘आइए..आइए यादवजी। विभाग में आपका स्वागत है।’’ ध्रुवलाल कुछ असहज हुए। इस तरह के औपचारिक माहौल के वे अभ्यस्त नहीं थे। उन्होंने गम्भीर होकर अंग्रेजी में ‘थैंक यू’ से मिलता-जुलता कुछ कहा।
कमरे में मौजूद आठ जोड़ा शातिर आँखों ने उनका मुआयना शुरू कर दिया था। बीच-बीच में ये आँखें एक-दूसरे को अपना मूल्यांकन भी दे रही थीं। है पट्ठा जोरदार ! ऐसा आदमी जो शरीर और भाषा से मजबूत हो और दिमाग से कमजोर, उनके लिए बड़े काम का था।
ऐसे समय में तबादला ! जितना कुछ खर्च करके वे यहाँ आए हैं, अभी तो दसवाँ हिस्सा भी नहीं निकला। बचत की तो बात ही क्या की जाए। इसलिए कमलाकान्त वर्मा, जिन्हें दफ्तर में सब लोग बड़े साहब कहते हैं, हतप्रभ हैं और दफ्तर का कमरा बन्द कर अपने विशेष मातहतों के साथ उस आदेश पर विचार-विमर्श कर रहे हैं जिसे अभी-अभी मुख्यालय का एक चपरासी थमा गया है।
कमरे में वर्मा साहब के अलावा चार लोग और थे। ये चार लोग अलग-अलग कामों से वहाँ मौजूद थे। एक कारण ऐसा था जो चारों की उपस्थित के पीछे था दफ्तर में सत्ता-परिवर्तन हो रहा था। ये चारों सत्ता पक्ष के लोग थे। नौकरशाही में भी राजनीति की तरह सत्ता परिवर्तित होते ही मुँह फेरने की परम्परा शुरू हो गई थी, पर ये लोग कुछ हयादार लगते थे, जो तबादले का आदेश आने के बाद भी मन्त्रणा के लिए उपलब्ध थे। या यह भी हो सकता है कि छोटे-मोटे बनाना रिपब्लिकों की तरह यहाँ भी अभी सब कुछ अनिश्चित था। तख्तापलट हो भी सकता है और यह भी हो सकता है कि शाहे-वक्त दुश्मन के हाथी-घोड़ों को रौंदता हुआ वापस गढ़ पर काबिज हो जाए। वैसे भी इस प्रदेश में नौकरशाही के तबादलों के हुक्म नीलाम होते थे। दिन में चार बार भी उनमें परिवर्तन हो सकता था। जो भी कारण हो ये चारों लोग तबादले का आदेश आने के बाद भी वहाँ थे और आदेश को बार-बार उलट-पुलटकर पढ़ रहे थे, फुसफुसाकर बातें कर रहे थे और बड़े साहब को अपनी बहुमूल्य राय दे रहे थे।
वर्मा साहब के बाईं तरफ थे रिजवानुल हक जो इस दफ्तर में सहायक अभियन्ता थे। पचास के पेटे में पहुंचा उनका शरीर बीमारी और दुर्घटनाओं के कारण लगभग ढल चुका था। माथे के ऊपर आधी सफाचट चाँद के कारण उनका पूरा व्यक्तित्व काफी गम्भीर किस्म का लगता था। वे कम बोलते थे और बिना माँगे कभी राय नहीं देते थे। दफ्तर में कोई भी बड़ा साहब आ जाए उनको इसी आदत के कारण अपना राजदार बना लेता था। लोगों को याद नहीं पड़ता था कि कभी किसी अधिशासी अभियन्ता से उनकी नहीं पटी हो।
जब कमलाकान्त वर्मा यहाँ आए तो कुछ दिनों तक उनसे भड़कते रहे। कारण सिर्फ यह था कि वे उनके पूर्वाधिकारी के करीब थे और पिछली बार जब वर्मा इसी तरह का आदेश कराकर लखनऊ से रवाना हुए तो उनके पूर्वाधिकारी ने अपने बँगले पर जो आपात बैठक बुलाई थी उसमें वे भी शरीक हुए थे। दफ्तर में कुछ दिनों तक हक साहब को बेचैन देखा गया। उनके विरोधियों ने चटखारे ले-लेकर वास्तविक, अर्द्ध वास्तविक और काल्पनिक खबरें प्रसारित कीं कि किस तरह हक साहब को बड़े साहब के कमरे में घुसने के पहले तीन घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती है या कि उनके पास अब कोई महत्त्वपूर्ण काम नहीं है या कि जल्दी ही बड़े साहब उन्हें डिजाइन सेक्शन में शंट कराने वाले हैं।
हक साहब इन सारी चर्चाओं से विचलित नहीं हुए। दफ्तर के अनुभवी बाबुओं की तरह उन्हें भी पता था कि यह तो अस्थायी दौर है। यह हर बार सत्ता परिवर्तन के साथ आता है, फिर कुछ महीनों में ठीक हो जाता है। इस बार भी यही हुआ। कभी ईद पड़ी, कभी बकरीद। हक साहब की बेगम अच्छा मुर्गा पकाती थीं और वर्मा साहब की पत्नी खाने की शौकीन थीं। पहली ईद पर हक बड़े साहब के बेरुखे मुबारकबाद के बावजूद दोहरे होते हुए बोले, ‘‘सर, मेरी फैमिली की बड़ी इच्छा थी कि मैडम और बच्चे हमारे गरीबखाने पर तशरीफ लाते पर आप इतने बिजी रहते हैं कि अर्ज करने की हिम्मत नहीं पड़ी और मैं खुद ही हाजिर हुआ हूँ। बेगम ने अपने हाथ से मुर्गा पकाया है। उम्मीद है बच्चों को पसन्द आएगा।’’
मुर्गा बच्चों को खूब पसन्द आया पर वर्मा साहब की फाँस अभी दूर नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों हक साहब की बेगम साहिबा किसी न किसी मौके पर मुर्गे या बकरे की कोई लजीज डिश बनाकर भेजती रहीं।
विरोधी खेमे का चपरासी बड़े साहब के घर पर तैनात था। उससे बात खुली तो यह खेमा चौकन्ना हुआ।
एक शाम जब दो टिफिन कैरियरों में भरकर मटन कोरमा, चिकन मुगलाई, मटन यखनी और सींक कबाब जैसी चीजों के साथ जानीवाकर ब्लैक लेबल की बोतल इस आग्रह के साथ पहुंची कि ‘सर मेरा साला कल सऊदी अरब से आया है। वही एयरपोर्ट से मेरे लिए ड्यूटी फ्री स्काच ले आया। अब मैंने तो छोड़ रखी है। साला ठहरा नमाजी, हाथ नहीं लगाता। बेगम ने कहा बड़े साहब इसकी कद्र जानते हैं, उन्हें यह तोहफा दे आओ। साथ में थोड़ा सा नान वेजिटेरिनयन बच्चों के लिए लेते जाओ। पता नहीं कैसा बना है। मेम साहब ने कभी राय नहीं दी, ‘‘विरोधी कैम्प सक्रिय हो गया। गुप्तचर छोड़े गए और जो सूचना वे लेकर आए उससे इस कैम्प की बाँछें खिल गईं।
दूसरे दिन बड़े साहब के कमरे में स्टाफ मीटिंग के दौरान जब चाय का मध्यान्तर हुआ तो हल्की-फुल्की बातों के दौरान सहायक अभियन्ता गुप्ता ने हक से ऐसे ही अनायास पूछ लिया, ‘‘भाभी को कब ला रहे हैं हक साहब ? कब तक मातादीन के हाथ का खाना खाएंगे।?’’
हक साहब ने चौंककर देखा। वे बोलते कम थे पर उनका दिमाग बड़ी तेज हरकत करता था। स्पष्ट था कि बड़े साहब को विरोधी खेमा यह बताने की कोशिश कर रहा है कि पिछले दो महीने से उनकी पत्नी अपने मायके बाराबंकी गई हुई हैं और वे करीम ढाबे से मुर्गा बनवाकर अपनी बेगम के नाम पर बड़े साहब को खिला रहे थे।
बड़े साहब ने चाय का प्याला नीचे रख दिया और हल्के से चश्मा हाथ में लेकर उसे रूमाल से पोंछने लगे।
‘‘बेगम तो बाराबंकी और यहाँ के बीच चक्कर लगाती रहती हैं। दरअसल, सर, जब से फादर-इन-ला की तबीयत खराब हुई है उन्हें दो जगह के इन्तजाम देखने पड़ रहे थे। एक ही भाई है उनका जो सऊदी अरब में है। जमींदारी है-छोड़ी भी नहीं जा सकती। बेगम को ही देखनी पड़ रही है। कल साला उन्हें लेकर आया था। आज फिर वापस गए हैं वे लोग।’’
विरोधी खेमे के लोग इस तरह मुस्कुराए कि किसी और को मुस्कान दिखाई दे न दे, बड़े साहब को जरूर दिखाई दे जाए।
अपने देश में पिछले कुछ सालों में और कोई तरक्की हुई हो या नहीं पर इलेक्टॉनिक एक्सचेंजों की बहार जरूर आ गई है। मोहल्ले-मोहल्ले में खुले पी.सी.ओ.में एक बार बाराबंकी के लिए सक्रिय हुआ और देर रात तक बेगम हक शहर में हाजिर हो गईं। विरोधी खेमा दूसरे दिन हतप्रभ रह गया, जब उसे पता चला कि मेम साहब की बीमारी की खबर, जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, सुनकर बेगम साहिबा बड़े साहब के घर अगले दिन दोपहर हालचाल पूछती देखी गईं। साथ में पिछले दिन से बड़ा टिफिन कैरियर था।
बाद में जैसा कि पिछले कई मौकों पर हुआ था और दफ्तर के अनुभवी बाबू पहले से जानते थे, वैसा ही हुआ। वे बड़े साहब की अन्तरंग टीम के सदस्य बन गए और उसी हैसियत से आज की मन्त्रणा में शरीक थे।
कमरे में वर्मा साहब के दाहिनी तरफ बैठे हुए व्यक्ति की उपस्थिति का कारण बड़ा दिलचस्प था। छोटे-छोटे बाल, गैंडे जैसी गर्दन और टूटे हुए कानवाले इन सज्जन को किसी अखाड़े में होना चाहिए था। वे दफ्तर में थे पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके जीवन का मूलमन्त्र था कि पूरा जीवन ही अखाड़ा है। वे कभी भी कहीं भी कुश्ती लड़ने के लिए तैयार रहते थे। चूँकि अपने जागृत समय का बड़ा हिस्सा वे दफ्तर में बिताते थे इसलिए मौजूदा जीवन की अधिकांश कुश्तियां भी वे यहीं लड़ते थे। अक्सर उनके साथ बातचीत करने वाले को उनकी कुश्ती कला से परिचित होने का अवसर मिलता था। धोबिया पाट उनका प्रिय दाँव था और दफ्तर के बरामदों में अगर कोई कर्मचारी, ठेकेदार या मुलाकाती लँगड़ाता हुआ दिखाई दे जाता तो बिना बताए लोग मान लेते कि वह व्यक्ति इनसे कुछ गम्भीर विचार-विमर्श करके जा रहा है।
ध्रुवलाल यादव नामक ये सज्जन जूनियर इंजीनियर थे और डॉ. रघुबीर जैसे उत्साही हिन्दी-प्रेमियों की मेहनत को धता बताते हुए लोग उन्हें अवर अभियन्ता न कहकर जे.ई. कहते थे। वे जे.ई. थे इसलिए जब तक बोलते या लिखते नहीं थे, लोग मानकर चलते थे कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जरूर हासिल किया होगा। जैसे ही उनके श्रीमुख से कोई वाक्य निकलता या वे कागज पर अपने पेशे से संबंधित कोई चीज लिखते, सामनेवाला मान लेता कि वे भी उन फैक्टरियों से निकला हुआ माल थे जिन्हें हमारे शिक्षाविद् स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या पालीटेक्नीक के नाम से पुकारते थे और जो धड़ाधड़ साल-दर-साल हजारों लाखों की तादाद में ध्रुवलाल जैसे होनहार निकालते रहते हैं। उन्होंने पालीटेक्नीक में पढ़ाई के अतिरिक्त प्रयुक्त होनेवाले दो तरीकों में से एक का प्रयोग करके डिप्लोमा हासिल किया था। उनके द्वारा प्रयुक्त तरीका विभाग में भी बड़ा काम आता है, यह उन्हें नौकरी शुरू करने पर ही पता चला।
जे.ई.ध्रुवलाल यादव के सामने जीवन की प्राथमिकताएँ शुरू से ही बड़ी स्पष्ट थीं। उनके बाप मझोले दर्जे के काश्तकार थे और लगभग बीस भैंस-गायों की सेवा-सुश्रुवा करके अपने परिवार को औसत भारतीय किसान की जिन्दगी से बेहतर जीवन प्रदान किए हुए थे। लेकिन ध्रुवलाल अपने परिवेश के मुकाबले ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। टखने-टखने तक गोबर में डूबकर गाय-भैसों की सेवा करना और शाम को कान पर हाथ रखकर बिरहा गाना-सिर्फ इन्हीं दो कामों तक वे अपनी जिन्दगी सीमित नहीं रख सकते थे। लिहाजा उन्होंने पढ़ने का फैसला किया। बाप के बहुत बच्चे थे। जमाना भी बदल रहा था। अपने लिए अब ‘करिया अच्छर भैंस बराबर’ सुनना बाप को खलने लगा था। इसलिए एक लड़के का पढ़ाई की तरफ रुझान उसके लिए खुशी की बात थी। उसने औपचारिक रूप से ससुरी महँगाई का जिक्र जरूर किया पर ध्रुवलाल को शहर भेज दिया।
बचपन से ही घी-दूध का सुख होने तथा बाप के प्रिय मुहावरे के अनुसार जूता मारकर सुबह-सुबह अखाड़े में ठेले जाने के कारण ध्रुवलाल एक अदद कसरती बदन के मालिक थे। उनका कद छह फुट से कुछ ऊपर था, दोनों तरफ से कान टूटे हुए थे, रंग गन्दुम और स्वर लट्ठमार हद तक उजड्ड था। यही सारी चीजें उनकी पूँजी थीं। सबसे पहले यह पूँजी पालीटेक्नीक में काम आई।
पालीटेक्नीक में पहुंचने के पहले दो-तीन हफ्ते में ही यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में छपी पाठ्य-पुस्तकें उनकी लिए ग्रीक और लैटिन के महाकाव्यों की तरह थीं।
ध्रुवलाल यादव के ईमानदार मन ने उन्हें सलाह दी कि भाग चल प्यारे ! कहाँ फँस गया ! जीवन इन किताबों से परे ज्यादा सुखद है। दर्जा आठ में किसी कवि ने, जिसका नाम स्वाभाविक था कि वे भूल गए थे, सही ही लिखा था कि अहा ! ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे। पर आगे काशी फल कूष्मांड के साथ-साथ भूसा, गोबर और बाप के जूते का ऐसा त्रिकोण फ्लैश बैक की तरह सामने आता कि वे तो वे उनका ईमानदार मन भी काँप जाता। उन्होंने अपने मन की अनसुनी कर दी और सफलता के गुर दूसरी जगह तलाशने शुरू कर दिए।
भारतीय समाज में बिरादरी बहुत बड़ा सम्बल है। ध्रुवलाल के काम भी यही सम्बल आया। पहले रैगिंग के समय भी यह सम्बल उनके साथ था। रैगिंग में तो उनका डील-डौल और टूटे हुए कान भी निपट लेते पर पढ़ाई में मामला कुछ दूसरा था। उनके बिरादरी के सीनियरों ने बताया कि सूबे के दूसरे पालीटेक्नीकों की तरह इस पालीटेक्नीक में भी सफलता के लिए पढ़ाई के अलावा दो रास्ते थे। पढ़ाई तो निरीह छात्र करते थे। ध्रुवलाल सरीखों को तो शेष दो रास्तों में से एक चुनना था।
पहला रास्ता था बाहुबल का और दूसरा था धनबल का। बाहुबली छात्र कट्टा या चाकू मेज पर रखते और आराम से किताबें खोलकर नकल करते। इन बाहुबली छात्रों की प्रतिभा सत्र के प्रारम्भ में ही पहचान ली जाती और अध्यापकों का कोई न कोई गुट उनके सिर पर वरद-हस्त रख देता। बाहुबली से यह गुट साल-भर अपने विरोधी अध्यापकों को पिटवाता या गाली दिलवाता और इत्महान में इन्हें पर्चा आउट करने से लेकर छोटी-छोटी पुर्जियों पर उतर लिखकर पहुँचाने तक का काम करता।
दूसरा रास्ता था धनबल का। जिस समय ध्रुवलाल पालीटेक्नीक में पहुंचे भारतीय समाज में बहुत कुछ बदल रहा था। शिक्षा की दुनिया बदल रही थी और उससे जुड़े गुरु बदल रहे थे। अब गुरु राजपुत्रों को दौड़ जिताने के लिए निर्धन शिष्यों के अँगूठे नहीं कटवाते थे। वे धनिक पुत्रों से वाजिब फीस लेकर उन्हें दौड़ शुरू होने से पहले ही आगे कर देते थे। प्रधानाध्यापकों और कॉलेजों के मैनेजरों ने नकल को एक व्यवस्थित रोगजार का रूप दे दिया था। हर चीज के रेट निर्धारित हो गए थे। यदि अपने तयशुदा कक्ष में नकल करनी थी तो उसकी एक कीमत थी, किसी अलग कमरे में बैठकर सहायक की मदद से उत्तर पुस्तिका लिखनी थी तो उसकी दूसरी कीमत थी, किसी दूसरे को बैठाकर उससे उत्तर पुस्तिका लिखवाने की कीमत अलग थी और अगर कोई छात्र चाहते कि विषय का अध्यापक ही उसके पास खड़ा होकर इमला दे तो इसकी फीस सबसे भिन्न थी।
ध्रुवलाल ने पहला रास्ता चुना। वे एक-एक कर सारी कक्षाएँ पास करते गए। यह रास्ता परीक्षा पास करने के अलावा नौकरी में भी उनके काम आया। प्रारम्भ में जब वे इस दफ्तर में आए उनकी छवि पहले ही यहाँ पहुंच चुकी थी। अपने सुगठित शरीर और उज़ड्ड जुबान के साथ वे एक ऐंटी इस्टैब्लिसमेंट छवि लिये दफ्तर में घुसे। नियुक्ति पत्र के मुताबिक जिस समय उन्हें वहाँ होना चाहिए था उससे वे सिर्फ पाँच महीने लेट थे। हुआ यह कि सरकारी नौकरी मिलने के पहले ही उन्हें कहीं विदेश में भी नौकरी दिलाने का भरोसा किसी एजेंट ने दिया था। अत: इस नौकरी का नियुक्ति-पत्र जेब में रखे वे विदेशी नौकरी के लिए दौड़ते रहे और अन्त में निराश होकर पाँच महीने बाद ज्वाइन करने इस दफ्तर में पहुँचे। पहुँचते ही उनके और बड़े बाबू के बीच में बड़ी संवैधानिक किस्म की बहस छिड़ गई। बड़े बाबू के मुताबिक कोई भी नियुक्ति-पत्र कुछ खास समय तक ही वैध रहता है। कम से कम पांच महीने तक तो नहीं ही रहता। उनकी राय में ध्रुवलाल यादव को फिर से जाकर अपने नियुक्ति-पत्र का नवीनीकरण कराना चाहिए था। इसके विपरीत ध्रुवलाल का मानना था कि एक बार नियुक्ति-पत्र मिलने के बाद रिटायरमेंट की उम्र तक प्रभावी रहता है। उन्होंने बड़े बाबू को चुनौती भी दी कि वे एक भी नियम ऐसा दिखा दें जिसके मुताबिक कोई नियुक्ति-पत्र पाँच महीने बाद रद्द हो जाता है। बड़े बाबू कोई भी ऐसा नियम नहीं दिखा पाये। फिर भी बड़े बाबू को धर्मसंकट से उबारने के लिए उन्होंने मीठे स्वर में आग्रह किया कि उन्हें पाँच महीने पहले की निर्धारित तारीख में ही ज्वाइन करा दिया जाए।
बड़े बाबू जो दप्तर के दूसरे बाबूओं की तरह उन्हें उनके सुगठित शरीर और मुंह में ठूँसे हुए पान के कारण ‘महिमा बरनि न जाए’ वाले भाव से निहार रहे थे, उनके इस आग्रह पर एकदम से बड़े बाबू बन गए। उन्होंने अपने तीस साल की बाबूगिरी का निचोड़ फाइनेंसियल हैंडबुक के फलाँ पेज और अलाँ पैरे तथा गवर्नमेंट सर्वेंट्स कांडक्ट रूल्स के पेज नं. इतने से इतने तक के उद्धरण के रूप में देना शुरू कर दिया जिसे ध्रुवलाल काफी अनिच्छा और अधैर्य के साथ झेलते रहे। इसीलिए पब्लिक सेक्टर इस मुल्क में असफल हो रहा है-उन्होंने निराशा से सोचा और हवा में मुँह उठाकर किसी काल्पनिक व्यक्ति की माँ-बहन के साथ अपने शारीरिक सम्बन्ध कायम करने लगे। बड़े बाबू अगर काफी मोटी चमड़ी के न होते तो इन सम्बोधनों को अपने लिए ही समझ लेते पर वे निर्विकार भाव से किसी फाइल में डूब गए। दूसरे बाबुओं ने जरूर आँखें मटकाईं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अपने उद्गारों से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि श्री ध्रुवलाल जिन स्त्रियों के सम्मान में कसीदे पढ़ रहे थे वे बड़े बाबू की ही पत्नी और बेटियाँ थी।
बड़े बाबू ने भारतीय नौकरशाही का मूल मन्त्र पकड़ा। जब कोई फैसला न करना हो तो फौरन फाइल पर लिखो-बात करें। यहाँ उनके नीचे कोई ऐसा नहीं था जिसके पास ‘प्लीज स्पीक’ लिखकर वे फाइल भेज सकते थे और यमदूत की तरह ध्रुवलाल सामने खड़े थे इसलिए वे भुनभुनाते हुए स्वयं ही उनका नियुक्ति पत्र लेकर उठ खड़े हुए और बड़े साहब के कमरे की तरफ बात करने के लिए बढ़ गए और दो-तीन घंटे तक नहीं लौटे।
इन दो-तीन घंटों का बड़े साहब के विरोधियों ने जमकर सदुपयोग किया। दूसरे दफ्तरों की तरह इस दफ्तर में भी काम होता हो या नहीं, राजनीति खूब होती थी। कौटिल्य ने सहस्रों वर्षों पूर्व राजनीति और गुप्तचरी का सम्बन्ध परिभाषित कर दिया था और यह दफ्तर पूरी श्रद्धा के साथ उस पर विश्वास करता था। सरकारी गुप्तचर एजेंसियों की तरह यहाँ गोपनीय सूचनाएँ अखबारों की करतनों से नहीं उपजती थीं बल्कि इन्हें हासिल करने के लिए मेहनत की जाती थी, इसलिए अक्सर इनमें कुछ दम भी होता था। ध्रुवलाल यादव का कमरे में प्रवेश, बड़े बाबू के साथ उनके नाटकीय संवाद और बाबुओं की प्रतिक्रिया के बीच अचानक जायसवाल नामक ठेकेदार क्यों ? बाबुओं की सेवा के लिए लाया गया मगही पान का आधे से ज्यादा भाग खोखा तिवारी बाबू की मेज पर छोड़कर कमरे से गायब हो गया, इसका पता करने के लिए अशोक कुमार शुक्ला सहायक अभियन्ता अर्थात् ए.ई.के कमरे में चलना पड़ेगा जो इस कमरे से तीन कमरे दूर था और जिसमें चौरसिया नामक एक अन्य ए.ई.भी बैठते थे और जो इस समय किसी साइट पर गए हुए थे। उनके न होने से ही ध्रुवलाल वहाँ निमन्त्रित किए गए थे। अगर वे होते तो यह गोष्ठी कहीं और होती क्योंकि उनके बारे में शुक्ला का मानना था कि वे बड़े साहब के गुप्तचर थे और उन्हें इस कमरे में बिठाया ही इसलिए गया था कि वे शुक्ला एंड कम्पनी पर निगरानी रख सकें।
इस कमरे में ध्रुवलाल यादव की दफ्तरी दीक्षा शुरू हुई।
कमरे में दो मेजें थीं। दो मेजें इसलिए थीं कि सिर्फ दो ही मेजें उसमें आ सकती थीं। दोनों मेजों के पीछे एक-एक कुर्सी थी। एक कुर्सी का एक हत्था उखड़ा हुआ था और पीछे के ताँत भी जगह-जगह से टूटे हुए थे, उस पर शुक्ला बैठे हुए थे। दूसरी कुर्सी घूमनेवाली थी और उस पर न सिर्फ मैली सी एक गद्दी थी बल्कि पीछे एक लिहाफ भी था जो शुरू में जरूर सफेद रहा होगा पर अब बदरंग हो चुका था। कुर्सियों की यह दशा दफ्तर में बड़े साहब से निकटता का पैमाना था।
दोनों मेजों के सामने दो कुर्सियाँ थीं। चार में से कोई कुर्सी साबुत नहीं थी। किसी के पीछे के ताँत टूटे थे और किसी के नीचे के, किसी हत्था हिल रहा था तो किसी के पांव डगमग कर रहे थे। मेजों पर बेतरतीब फाइल कवर कागज पेपरवेट और पान के खोखे फैले हुए थे। पूरे कमरे में सिगरेट के टुकड़े और राख बिखरी हुई थी और कमरे के हर कोने में दीवारें पान की पीक से अमूर्त चित्रकला का नमूना पेश कर रही थीं। दफ्तर में बड़े साहब के कमरे को छोड़कर सभी कमरों की ऐसी ही हालत थी और इस कमरे में भी दूसरे कमरों की तरह सरकारी काम के अलावा सब कुछ होता था।
इसी कमरे में ध्रुवलाल यादव नौकरशाही में दीक्षित हुए। उन्हें चौरसिया ठेकेदार कनखियों से इशारा करते हुए यहाँ तक ले आया था।
कमरे में शुक्ला नामक सहायक अभियन्ता या ए.ई. के अलावा दो जे.ई. और एक बाबू पहले से थे। छोटे से कमरे में उन्होंने सामने पड़ी कुर्सियों का रुख इस तरह मोड़ लिया था कि पहली बार घुसने पर किसी गोलमेज सम्मेलन का सा माहौल लगता था। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, ध्रुवलाल ने चौथी खाली पड़ी कुर्सी पर कब्जा कर लिया। जायसवाल ने चारों तरफ इस प्रकार देखा मानो उसकी दृष्टि से वहां कोई कुर्सी उत्पन्न हो जाएगी। अभी उसकी हैसियत ऐसी नहीं थी कि शुक्ला उसे चौरसिया की कुर्सी पर बैठने को कहते इसलिए थोड़ी देर इधर-उधर देखकर वह ‘अभी पान लेकर होता हूँ, जैसा कोई वाक्य बुदबुदाकर अदृश्य हो गया।
‘‘आइए..आइए यादवजी। विभाग में आपका स्वागत है।’’ ध्रुवलाल कुछ असहज हुए। इस तरह के औपचारिक माहौल के वे अभ्यस्त नहीं थे। उन्होंने गम्भीर होकर अंग्रेजी में ‘थैंक यू’ से मिलता-जुलता कुछ कहा।
कमरे में मौजूद आठ जोड़ा शातिर आँखों ने उनका मुआयना शुरू कर दिया था। बीच-बीच में ये आँखें एक-दूसरे को अपना मूल्यांकन भी दे रही थीं। है पट्ठा जोरदार ! ऐसा आदमी जो शरीर और भाषा से मजबूत हो और दिमाग से कमजोर, उनके लिए बड़े काम का था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book