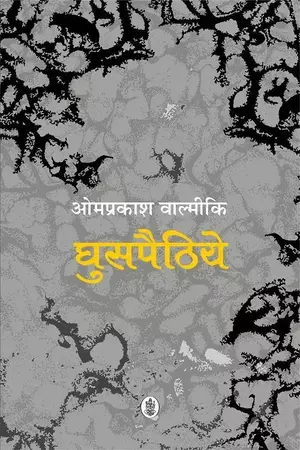|
कहानी संग्रह >> घुसपैठिये घुसपैठियेओमप्रकाश वाल्मीकि
|
345 पाठक हैं |
|||||||
"सच और मानवता से बुनी प्रतिरोध की आवाज़।"
Ghupaitiye
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
ओमप्रकाश वाल्मीकि के इस संग्रह की तमाम कहानियाँ दलित संदर्भों से जुड़ी हुई हैं। यह दलित जीवन का यथार्थ है जिसे कहानीकार ने इन कहानियाँ ने इन कहानियों में निहायत ही संजीदगी से, यथार्थ के प्रति वस्तुनिष्ठ रखते हुए, कहानी के रचना-विधान की संगति में दृष्टिकोण के समूचे खुलेपन के साथ चित्रित किया है। ये भेधक और मार्मिक कहानियाँ हैं।
व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश, कथा-विन्यास के अनुरुप तर्क और विचार, अनुभवजन्य ये कहानियाँ दलितों के सुख-दुःख, उनकी मुखरता और संघर्ष की कहानियाँ हैं। वस्तुगत यथार्थ की संगति में जिस रचनात्मक कौशल के साथ इन कहानियों को ओमप्रकाश वाल्मीकि इस बिन्दु तक लाए हैं वह उनके कहानीकार की ताकत का साक्ष्य है। इन कहानियों में दलित और स्त्री की पीड़ाएँ मिलकर एक हो गई हैं। ओमप्रकाश वाल्मीकि में विवश, आंतरिक घृणा का यह विस्फोट सृजनात्मक ऊर्जा का स्त्रोत है।
ये कहानियाँ केवल दलित लेखन के दायरे की ही कहानियाँ नहीं हैं बल्कि उनमें रचना-सामर्थ्य और उनकी सोच के जो पहलू उभरे हैं वे उन्हें हिन्दी की यथार्थवादी कहानी की परम्परा का कहानीकार सिद्ध करते हैं।
ओमप्रकाश वाल्मीकि कहानी के शिल्प, अंतर्वस्तु, सौन्दर्य तथा पाठक पर उसके समग्र प्रभाव का ध्यान रखने वाले रचनाकार हैं।
व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश, कथा-विन्यास के अनुरुप तर्क और विचार, अनुभवजन्य ये कहानियाँ दलितों के सुख-दुःख, उनकी मुखरता और संघर्ष की कहानियाँ हैं। वस्तुगत यथार्थ की संगति में जिस रचनात्मक कौशल के साथ इन कहानियों को ओमप्रकाश वाल्मीकि इस बिन्दु तक लाए हैं वह उनके कहानीकार की ताकत का साक्ष्य है। इन कहानियों में दलित और स्त्री की पीड़ाएँ मिलकर एक हो गई हैं। ओमप्रकाश वाल्मीकि में विवश, आंतरिक घृणा का यह विस्फोट सृजनात्मक ऊर्जा का स्त्रोत है।
ये कहानियाँ केवल दलित लेखन के दायरे की ही कहानियाँ नहीं हैं बल्कि उनमें रचना-सामर्थ्य और उनकी सोच के जो पहलू उभरे हैं वे उन्हें हिन्दी की यथार्थवादी कहानी की परम्परा का कहानीकार सिद्ध करते हैं।
ओमप्रकाश वाल्मीकि कहानी के शिल्प, अंतर्वस्तु, सौन्दर्य तथा पाठक पर उसके समग्र प्रभाव का ध्यान रखने वाले रचनाकार हैं।
भूमिका
‘सलाम’ के बाद मेरा यह दूसरा कहानी-संग्रह है। अपनी कहानियों पर चर्चा करना, उनमें फिर से लौटना तकलीफदेह लगता है। क्योंकि छपने के बाद अपनी कहानियों को फिर से पढ़ना कभी भी मुझे उत्साहवर्धक नहीं लगा। कभी-कभी अपना ही लिखा हुआ अपना नहीं लगता।
इन कहानियों की अन्तर्वस्तु मेरे अनुभव-जगत की त्रासदियों और दुःखों से उपजी सामाजिक संवेदनाएँ हैं। जिन्हें शब्द-दर-शब्द गहरे अवसादों के साथ यन्त्रणा से गुजरते हुए लिखा है। कुछ संस्कारवान आलोचकों को यह सब अतिरेकपूर्ण और जातिवादी लगता है। विशेष रूप से उन्हें जो साहित्य में तथाकथित सार्वभौमिकता और शाश्वत सत्यों की बात करते हैं।
कई लेखक मित्रों को मेरी कहानियों में दलित पात्रों की मुखरता भयभीत करती है, तो कुछ को यह सब राजनीति प्रेरक भी लगता है। कई मित्र इसे काल्पनिक और अविश्वसनीय कहकर खारिज भी कर देने की कोशिश करते हैं।
कई विद्वानों, आलोचकों ने मेरी कहानियों के भीतर सुगबुगाती पीड़ा और दुःख-भरे संसार को समझने की कोशिश भी की है। राजेन्द्र यादव, नामवर सिंह, डॉक्टर शिवकुमार मिश्र, कंवल भारती, डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर शम्भू गुप्त, डॉक्टर मूलचन्द गौतम, भालचन्द्र जोशी तथा अनेक लेखकों ने मेरी कहानियों की अंतःचेतना की पड़ताल कर सामाजिक सरोकारों की पक्षधरता का सवाल उठाया है। मेरे लिए यह सब अनुभूति और अभिव्यक्ति की संवेदना का प्रश्न है। जो मेरे निजी जीवन तक ही सीमित नहीं है।
कई आलोचकों ने मेरी कहानियों में पात्रों द्वारा ‘गाली’ दिए जाने की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। कुछ हद तक वे इन गालियों को अश्लीलता के दायरे में देखते हैं।
सच तो यह है कि मैंने जैसा जीवन देखा-भोगा, महसूस किया, वैसा ही लिखने की, दिखाने की कोशिश की। मेरे इर्द-गिर्द की दुनिया अश्लील है तो इस अश्लीलता को मैं शब्दों के किस आवरण से छिपाने की कोशिश करता ? जीवन की नग्नता मात्र शब्दों से अभिव्यक्त नहीं होती है, स्थितियाँ और सामाजिक मान्यताएँ भी अश्लील होती हैं, जिनका सीधा ताल्लुक संस्कारों और परिवेश से होता है।
आरम्भिक दौर में कविताओं से ही मेरी कहानियाँ जन्मी हैं। कविताएँ पढ़ते हुए, लिखते हुए, अचानक कहानियाँ लिखी गईं। यह आज भी जारी है।
मेरी कहानियाँ जीवन के उन तमाम पहलुओं से जुड़ी हैं जो दलित जीवन के इर्द-गिर्द फैला हुआ है। ‘शवयात्रा’ कहानी इंडिया टुडे (22 जुलाई, 1998) में छपी थी। इस कहानी को लेकर कई दलित आलोचकों, लेखकों के अन्तर्विरोध जिस तरह खुलकर सामने आए, वह सब पीड़ादायक है। इसी तरह ‘घुसपैठिये’, ‘दिनेशपाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन’ कहानियाँ लिखते समय गहन यातना के क्षोभ से गुजरना पड़ा था।
दलित मानसिकता और सोच में जो गुणात्मक परिवर्तन विकसित हो रहे हैं, उनकी झलक ‘कूड़ाघर’ और ‘मुंबई कांड’ कहानियों में दिखाई देगी। ‘मैं ब्राह्मण नहीं हूँ’ कहानी राष्ट्रीय सहारा (10 सितम्बर, 2000) में छपी थी। पाठकों ने इसकी फोटो प्रतियाँ करके अनेक लोगों तक पहुँचाई थीं।
पाठकों ने मुझे विश्वास ही नहीं हौसला भी दिया है। निराशा के क्षणों में पाठकों ने सम्बल देकर ऊबारा भी है। साथ ही मेरी कमजोरियों की ओर इशारा भी किया है।
हंस, राष्ट्रीय सहारा, वसुधा, कथाक्रम, वर्तमान साहित्य, इतवारी पत्रिका, अक्षरा, भारत अश्वघोष, जनसत्ता, पंजाब केसरी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके द्वारा मेरी ये कहानियाँ असंख्य पाठकों तक पहुँची।
इस संग्रह की पांडुलिपि तैयार करने में श्री राजपाल सिंह ने जो तत्परता दिखाई और सहयोग दिया, मैं हृदय से उसका आभारी हूँ।
देहरादून
5 मार्च, 2003
इन कहानियों की अन्तर्वस्तु मेरे अनुभव-जगत की त्रासदियों और दुःखों से उपजी सामाजिक संवेदनाएँ हैं। जिन्हें शब्द-दर-शब्द गहरे अवसादों के साथ यन्त्रणा से गुजरते हुए लिखा है। कुछ संस्कारवान आलोचकों को यह सब अतिरेकपूर्ण और जातिवादी लगता है। विशेष रूप से उन्हें जो साहित्य में तथाकथित सार्वभौमिकता और शाश्वत सत्यों की बात करते हैं।
कई लेखक मित्रों को मेरी कहानियों में दलित पात्रों की मुखरता भयभीत करती है, तो कुछ को यह सब राजनीति प्रेरक भी लगता है। कई मित्र इसे काल्पनिक और अविश्वसनीय कहकर खारिज भी कर देने की कोशिश करते हैं।
कई विद्वानों, आलोचकों ने मेरी कहानियों के भीतर सुगबुगाती पीड़ा और दुःख-भरे संसार को समझने की कोशिश भी की है। राजेन्द्र यादव, नामवर सिंह, डॉक्टर शिवकुमार मिश्र, कंवल भारती, डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर शम्भू गुप्त, डॉक्टर मूलचन्द गौतम, भालचन्द्र जोशी तथा अनेक लेखकों ने मेरी कहानियों की अंतःचेतना की पड़ताल कर सामाजिक सरोकारों की पक्षधरता का सवाल उठाया है। मेरे लिए यह सब अनुभूति और अभिव्यक्ति की संवेदना का प्रश्न है। जो मेरे निजी जीवन तक ही सीमित नहीं है।
कई आलोचकों ने मेरी कहानियों में पात्रों द्वारा ‘गाली’ दिए जाने की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। कुछ हद तक वे इन गालियों को अश्लीलता के दायरे में देखते हैं।
सच तो यह है कि मैंने जैसा जीवन देखा-भोगा, महसूस किया, वैसा ही लिखने की, दिखाने की कोशिश की। मेरे इर्द-गिर्द की दुनिया अश्लील है तो इस अश्लीलता को मैं शब्दों के किस आवरण से छिपाने की कोशिश करता ? जीवन की नग्नता मात्र शब्दों से अभिव्यक्त नहीं होती है, स्थितियाँ और सामाजिक मान्यताएँ भी अश्लील होती हैं, जिनका सीधा ताल्लुक संस्कारों और परिवेश से होता है।
आरम्भिक दौर में कविताओं से ही मेरी कहानियाँ जन्मी हैं। कविताएँ पढ़ते हुए, लिखते हुए, अचानक कहानियाँ लिखी गईं। यह आज भी जारी है।
मेरी कहानियाँ जीवन के उन तमाम पहलुओं से जुड़ी हैं जो दलित जीवन के इर्द-गिर्द फैला हुआ है। ‘शवयात्रा’ कहानी इंडिया टुडे (22 जुलाई, 1998) में छपी थी। इस कहानी को लेकर कई दलित आलोचकों, लेखकों के अन्तर्विरोध जिस तरह खुलकर सामने आए, वह सब पीड़ादायक है। इसी तरह ‘घुसपैठिये’, ‘दिनेशपाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन’ कहानियाँ लिखते समय गहन यातना के क्षोभ से गुजरना पड़ा था।
दलित मानसिकता और सोच में जो गुणात्मक परिवर्तन विकसित हो रहे हैं, उनकी झलक ‘कूड़ाघर’ और ‘मुंबई कांड’ कहानियों में दिखाई देगी। ‘मैं ब्राह्मण नहीं हूँ’ कहानी राष्ट्रीय सहारा (10 सितम्बर, 2000) में छपी थी। पाठकों ने इसकी फोटो प्रतियाँ करके अनेक लोगों तक पहुँचाई थीं।
पाठकों ने मुझे विश्वास ही नहीं हौसला भी दिया है। निराशा के क्षणों में पाठकों ने सम्बल देकर ऊबारा भी है। साथ ही मेरी कमजोरियों की ओर इशारा भी किया है।
हंस, राष्ट्रीय सहारा, वसुधा, कथाक्रम, वर्तमान साहित्य, इतवारी पत्रिका, अक्षरा, भारत अश्वघोष, जनसत्ता, पंजाब केसरी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके द्वारा मेरी ये कहानियाँ असंख्य पाठकों तक पहुँची।
इस संग्रह की पांडुलिपि तैयार करने में श्री राजपाल सिंह ने जो तत्परता दिखाई और सहयोग दिया, मैं हृदय से उसका आभारी हूँ।
देहरादून
5 मार्च, 2003
ओमप्रकाश वाल्मीकि
घुसपैठिये
मेडिकल कॉलेज के छात्र सुभाष सोनकर की खबर से शहर की दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। अखबारों ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था। एक ही साल में यह दूसरी मौत थी मेडिकल कॉलेज में। फाइनल वर्ष की सुजाता की मौत को भी आत्महत्या का केस कहकर रफा-दफा कर दिया गया था। किसी ने भी आत्महत्या के कारणों की पड़ताल करना जरूरी नहीं समझा था। लगता था जैसे इस शहर की संवेदनाओं को लकवा मार गया है। दो-दो हत्याओं के बाद भी यह शहर गूँगा ही बना रहा।
राकेश के दफ्तर पहुँचते ही फोन की घंटी बजी। रमेश चौधरी का फोन था। उसने काँपती आवाज में कहा था, ‘‘राकेश साहब, सुभाष सोनकर बलि चढ़ गया है...’’
‘‘क्या ?...’’ राकेश ने लगभग चीखते हुए पूछा।
‘‘अभी और कितनी हत्याएँ होंगी राकेश साहब ?...’’ रमेश ने अपनी बात जारी रखी थी, ‘‘आखिर सोनकर का अपराध क्या था ?...सिर्फ इतना की माँ-बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे।’’ रमेश चौधरी का एक-एक शब्द गहरी वेदना से बाहर आ रहा था।
राकेश काठ की तरह जड़ हो गया था। रमेश चौधरी की भर्राई आवाज जैसे हजारों मील दूर से आ रही थी। जिसे वह ठीक से सुन नहीं पा रहा था। सोनकर की मौत का राकेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था। राकेश को लग रहा था जैसे रमेश चौधरी किसी गहरी खाई में खड़ा है। जहाँ से प्रतिध्वनित होकर आ रही आवाज धीमी हो गई थी। जिसे सुन पाना राकेश के लिए कठिन महसूस हो रहा था।
सुभाष सोनकर का उदास चेहरा राकेश की आँखों के सामने बार-बार आ रहा था। उसे लगा फोन उसकी पकड़ से फिसल रहा है।
उसकी स्मृति में वह दिन दस्तक देने लगा, जब रमेश चौधरी सुभाष सोनकर और उसके मित्रों को लेकर आया था।
उस रोज वह दफ्तर से घर आते ही अखबार लेकर बैठ गया था। रसोई में इन्दु की खटर-पटर चल रही थी। बच्चे दूसरे कमरे में अपना होमवर्क कर रहे थे। घर का वातावरण शान्त था, लेकिन दफ्तर से आते ही अखबार से चिपक जाना इन्दू को चिढ़ाने के लिए काफी था। उसने व्यंग्य से पूछा, ‘‘कहीं जाना है क्या ?’’
‘‘नहीं...क्यों ?’’ राकेश हड़बड़ा गया था।
‘‘कपड़े नहीं बदले...?’’ इन्दू ने शंका जाहिर की।
राकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। दरअसल वह कुछ बेचैन था। दफ्तर में रमेश चौधरी का फोन आया था। कुछ जरूरी बात करना चाहता था। शाम को घर आएगा। राकेश ने टालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रमेश चौधरी माना ही नहीं था। राकेश ने कहा भी था, ‘‘दफ्तर में ही आ जाओ।’’ लेकिन रमेश चौधरी ने कहा था, ‘‘नहीं, बात कुछ ऐसी ही है जो दफ्तर में नहीं हो सकती है।’’
रमेश चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता है। अक्सर किसी न किसी बहाने वह राकेश के पास आता ही रहता है। जब भी वह आता है राकेश अव्यवस्थित हो उठता है। उससे जितना बचने का प्रयास करो, वह उतना ही पीछे पड़ा रहता है। रमेश चौधरी के बोलने का अन्दाज कुछ ऐसा था कि सामनेवाला व्यक्ति सहज नहीं रह पाता था।
‘‘...तुम लोग अपने आपको समझते क्या हो ? तुम लोगों को सिर्फ बड़े-बड़े प्रमोशन चाहिए, वे भी आरक्षण के भरोसे। बच्चों को स्कूल-कॉलेज में एडमीशन भी कोटे से ही चाहिए। लेकिन इस कोटे को बचाए रखने के लिए जब कुछ करने की नौबत आती है तो तुम लोगों को जरूरी काम निकल आते हैं या फिर दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती। तब रमेश चौधरी ही बनेगा बलि का बकरा। गालियाँ भी वही खाएगा। देखो साहब...अगर भीड़ का हिस्सा बनने में आप लोगों को खतरा दिखाई देता तो ऐसी संस्थाओं को चंदा दो जो तुम्हारे हितों के लिए काम करती हैं...तुम लोग इसी तरह उदासीन बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब आरक्षण को ये लोग हजम कर जाएँगे....बाबा साहब तो हैं नहीं...और बाबा साहब के नुमाइन्दे बनने का जो ढोंग कर रहे हैं वे भी संसद में पहुँचते ही गीदड़ बनकर उनकी गोद में बैठ जाते हैं जो आरक्षण विरोधी हैं, और तरह-तरह की नौटंकियाँ करने में माहिर हैं। न्यायाधीशों से फैसले दिलवाएँगे कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग में आरक्षण से दाखिला नहीं मिलेगा। इससे प्रतिभाएँ नष्ट होती हैं...जैसे प्रतिभाएँ इनकी गुलाम हैं और सिर्फ इनके घरों में ही जन्मती हैं...अरे इतने ही प्रतिभावान थे तो देश की यह हालत कैसे हो गई...’’
ऐसे संवादों से राकेश आएँ-बाएँ देखने लगता है। और यदि यह वार्तालाप घर में चल रहा होता तो इन्दु को लगता है जैसे अडो़सी-पड़ोसी कान लगाकर सुन रहे हैं। इस वार्तालाप से इन्दु ऐसी उखड़ती है कि कई-कई दिन तक घर में गोलाबारी चलती ही रहती है। ऐसे में राकेश एकतरफा युद्धधविराम घोषित करके आत्मसमर्पण की मुद्रा अख्तियार कर लेता है।
इन्दु घुमा-फिराकर यही कहती है :
‘‘...तुम चाहे जितने बड़े अफसर बन जाओ, मेल-जोल इन लोगों से ही रखोगे, जिन्हें यह तमीज भी नहीं है कि सोफे पर बैठा कैसे जाता है...तुम्हें इनसे यारी-दोस्ती करना है तो घर से बाहर ही रखो...आस पड़ोस में जो थोड़ी-बहुत इज्जत है, उसे भी क्यों खत्म करने पर तुले हो...गले में ढोल बाँधकर मत घूमो...यह जो सरनेम लगा रखा है...यही क्या कम है...कितनी बार कहा है कि इसे बदलकर कुछ अच्छा-सा सरनेम लगाओ...बच्चे बड़े हो रहे हैं...इन्हें कितना सहना पड़ता है। कल पिंकी की सहेली कह रही थी...रैदास तो जूते बनाता था...तुम लोग भी जूते बनाते हो...पिंकी रोते हुए घर आई थी...मेरा तो जी करता है बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊँ...’’ इन्दु की यह तानाकशी राकेश को बौना बना देती है। वह खुद अपराध बोध से भर जाता है।
बस अखबार खोलकर बैठ जाता है। ऐसे अखबार की सुर्खियाँ गड्डमड्ड होकर काले धब्बों में बदल जाती हैं। और राकेश को लगने लगता है जैसे वह सुरक्षित है।
दरवाजे की घंटी बजने से उसकी विचार तन्द्रा टूट गई थी। उसने दरवाजा खोला। रमेश चौधरी ही था। उसके साथ चार युवा और थे। वे सब अन्दर आकर इधर-उधर पसर गए थे। राकेश उन्हें गौर से देख रहा था। सभी के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उदास चेहरों पर भय की परछाइयाँ दिखाई पड़ रही थीं।
वे सभी चुप थे। सभी अपने-अपने खोल में सिमटे हुए थे। खोल से बाहर आने की छटपटाहट उनके चेहरों से ज्यादा उनकी आँखों में थी। उनकी दशा देखकर राकेश के मन में कई तरह की शंकाएँ पनपने लगी थीं।
रमेश चौधरी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ‘‘राकेश साहब, यह है अमरदीप, ये विकास चौधरी, ये नितिन मेश्राम और ये सुभाष सोनकर। सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। अमरदीप और नितिन मेश्राम फाइनल वर्ष में हैं और ये दोनों प्रथम वर्ष में हैं। आपसे मिलना चाहते थे।’’
‘‘हाँ...जरूर...’’राकेश ने सहज भाव से कहा।
अमरदीप हिचकते हुए बोला, ‘‘सर ! हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं...समझ नहीं आ रहा है क्या करें ?’’ अमरदीप पल-भर के लिए रुका। खुद को व्यवस्थित करते हुए बोला, ‘‘मेडिकल कॉलेज के जो हालात हैं, उसमें हमारे लिए पढ़ाई जारी रखना दिन-प्रतिदिन कठिन हो रहा है। ये साल हमने जिन यातनाओं के साथ गुजारे हैं...हम ही जानते हैं। कई बार तो लगता था पढ़ाई छोड़कर वापस लौट जाएँ...लेकिन माँ-बाप की उम्मीदें रास्ता रोककर मजबूर कर देती हैं। उन सब यातनाओं के साथ पढ़ाई जारी रखना...बहुत तकलीफदेह है...एक रोज तो मैंने आत्महत्या तक करने का निश्चय कर लिया था।’’ निराशा और हताशा से लबरेज अमरदीप के शब्दों ने साँझ के धुँधलकों को और अधिक गहरा दिया था। अमरदीप के अन्तस से गूँजती चीत्कारें साफ-साफ सुनाई पड़ रही थीं।
माहौल गमगीन हो गया था। राकेश के हृदय में जैसे कम्पन बढ़ गए थे। अपने ही अन्तर्मन की हिलोरों पर तैरता अमरदीप बोला, ‘‘कल पूरा दिन होस्टल के एक कमरे में विकास चौधरी और सुभाष सोनकर को दरवाजा बन्द करके पीटा गया।’’
‘‘क्यों...? क्या रैगिंग चल रही थी ?’’ राकेश ने हैरानी से पूछा।
‘रैगिंग होती तो फर्स्टइयर के सभी छात्रों के साथ यह सुलूक होता। लेकिन वहाँ तो सिर्फ इन दोनों को ही पीटा गया,’’ अमरदीप ने जोर देकर कहा।
‘दलित छात्रों को अलग खड़ा करके अपमानित करना तो रोज का किस्सा है। प्रवेश परीक्षा के प्रतिशत अंक पूछकर थप्पड़ या घूँसों से प्रहार होता है। जरा भी विरोध किया तो लात पड़ती है। यह दो-चार दिन नहीं साल के साल चलता है। और यह पिटाई कॉलेज या छात्रावास तक ही सीमित नहीं है। शहर से कॉलेज तक जानेवाली बस में भी पिटाई होती है। कोई एक सीनियर चलती बस में चिल्लाकर कहता है, ‘‘इस बस में जो भी चमार स्टूडैंट है...वह खड़ा हो जाए...फिर उसे धकियाकर पिछली सीटों पर ले जाया जाता, जहाँ पहले से बैठे सीनियर लात, घूँसो से उसका स्वागत करते हैं।’’ अमरदीप ने हालात का ब्यौरा दिया।
‘‘यह तो सरासर जुल्म है,’’ राकेश ने उत्तेजित होते हुए कहा। अमरदीप ने राकेश की ओर देखा,...‘‘अभी कुछ दिन पहले ऐसी ही बस में फाइनल के प्रणव मिश्रा ने चिल्लाकर अवाज लगाई तो उस बस में सुभाष सोनकर था, जो प्रणव की आवाज पर चुपचाप रहा। सोनकर के पास जो छात्र बैठा था, उसने इशारे से बता दिया कि सोनकर यहाँ बैठा है। प्रणव मिश्रा अपनी अवहेलना पर तिलमिला गया। सोनकर के बाल पकड़कर अपनी ओर खींचे, ‘क्यों बे चमरटे सुनाई नहीं पड़ा हमने क्या कहा था ?’ सोनकर ने अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की...मैं चमार नहीं हूँ। बालों की पकड़ मजबूत थी। सोनकर कराह उठा। प्रणव मिश्रा का झन्नाटेदार थप्पड़ सोनकर के गाल पर पड़ा...(गाली)...चमार हो या सोनकर...ब्राह्मण तो नहीं हो...हो तो सिर्फ कोटेवाले...बस इतना ही काफी है, प्रणव मिश्रा ने सोनकर को लात-घूँसों से अधमरा कर दिया। पूरी बस में ठहाके गूँज रहे थे...बाबा साहब के नाम पर गालियाँ दी जा रही थीं। प्रणव मिश्रा के इस शौर्य पर उसे शाबाशियाँ मिल रही थीं।’’
राकेश ने सोनकर की ओर देखा। वह अपराधी की मुद्रा में सिर झुकाए बैठा था। सोनकर के चेहरे पर चोट के निशान और गहरे हो गए थे।
रमेश चौधरी भी खामोश था। लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियाँ कसी हुई थीं। चेहरे का रंग बदल रहा था। रसोई में इन्दु की खटर-पटर और तेज हो गई थी। इन्दु के खँखारने का स्वर राकेश के लिए संकेत था....‘अजी, आप इन पचड़ों में न पड़ो।’ रसोई के कामकाज के दौरान भी इन्दु के कान इन लोगों की बातचीत पर ही लगे थे।
इन्दु का जो नजरिया था, वह सामाजिक प्रताणना का प्रतिफल था। वह एक सहज जीवन जीना चाहती थी। उसे लगता था राकेश को इन झमेलों से बचना चाहिए। वह इसी कोशिश में लगी रहती थी कि आस-पड़ोस के लोग उनके बारे में न जान पाएँ कि वे कौन हैं ? उसे यह सब बहुत सुरक्षित लगता था। लेकिन राकेश उनकी व्यथा-कथा से विचलित हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि वे सब किसी घने बियाबान जंगल में फँस गए हैं जहाँ चारों ओर सिर्फ अँधेरा है या कँटीले झाड़-झंखाड़।
इन्दु रसोईं से निकलकर बेडरूम में चली गई थी। जहाँ बच्चे अपने होमवर्क में मशगूल थे। कुछ ही क्षण बाद राकेश का आठ वर्षीय पुत्र बाहर आया। आदेशात्मक लहजे में राकेश से बोला, ‘‘पापा ! मेरा होमवर्क कराओ।’’
‘‘हाँ, बेटे, बस अभी कराते हैं, दस मिनट में....जरा रमेश अंकल से बात कर लें...तब तक तुम अपनी ड्राइंग बना लो,’’ राकेश ने उसे बहला-फुसलाकर वापस भेज दिया। राकेश इन्दु का इशारा समझ रहा था—‘इन्हें जल्दी भगाओ...इन झंझटों से अपने आपको दूर रखो।’
राकेश कुछ अटपटा-सा गया था। रमेश चौधरी ने भी इशारा समझ लिया था। वह सहज बने रहना चाहता था। उसने राकेश को धीरे से कहा, ‘‘साहब, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे...बस इन लड़कों को कोई रास्ता सुझाइए....डॉक्टर तो इन्हें बनना ही है....।’’
राकेश गहरी सोच में था। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि इन हालात में छात्रों को क्या करना चाहिए।
नितिन मेश्राम अभी तक चुप था। राकेश को गहरी सोच में डूबा देखकर बोला, ‘‘होस्टल नं. एक में कमरा एलॉट हो जाने के बाद किसी दलित छात्र को उसमें घुसने नहीं दिया जाता है। घूम-फिरकर होस्टल नं. दो में ही दलित छात्रों को रखा जाता है। यही स्थिति गर्ल्स होस्टल की भी है। वहाँ की सभी दलित लड़कियाँ एक ही होस्टल में रहती हैं। कॉलेज मैनेजमेंट को ये समस्याएँ गंभीर नहीं लगतीं। उन्हें लगता है दलितों के लिए मेडिकल में आना अतिक्रमण करना है। जब उनसे शिकायत करते हैं तो ध्यान ही नहीं देते।’’
नितिन मेश्राम मुखर हो उठा था, ‘‘इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में भी भेदभाव बरता जाता है। प्रणव मिश्रा मेरे ही बैच में है। न क्लासेज अटेंड करता है, न प्रैक्टिकल। फिर भी त्रिवेदी सर उसे ही सबसे ज्यादा अंक देते हैं। अटैंडेंस की भी समस्या नहीं होती।’’ मेश्राम ने कटुता से कहा।
राकेश की स्मृतियों में अतीत दस्तक देने लगा था। जब वह पहली बार होस्टल गया था। उसे जो रूम एलॉट हुआ था उसमें पहले से एक छात्र था जिसने उसे अपने कमरे में घुसने ही नहीं दिया था। उसने साफ मना कर दिया था कि वह किसी भंगी-चमार के साथ अपना रूम शेयर नहीं कर सकता है। जब उसने होस्टल वार्डन से शिकायत की तो उसने भी उसकी जाति पूछी थी और उसे एक दलित छात्र के साथ रख दिया था। साथ ही उसे चेतावनी भी दी थी—‘अपनी औकात में रहो...वरना बाहर कर दूँगा।’
छात्रावास जीवन के दिन बहुत ही पीड़ादायक थे। एक-एक दिन जैसे यन्त्रणा से गुजर कर पार करना पड़ता था। मैस में भी अलग बैठना पड़ता था।
रमेश चौधरी ने राकेश की सोच को झटका दिया, ‘‘साहब, अब आप ही बताइए क्या किया जाए ?’’
‘‘तुम लोग डीन से मिले ?’’ राकेश ने सवाल किया।
‘‘जी, मिले थे...उनका कहना है—आरक्षण से आए हो थोड़ा-बहुत तो सहना ही होगा। सवर्ण छात्रों की ज्यादतियों को वे अनुचित नहीं मानते। क्योंकि नाइंसाफी के खिलाफ ये प्रतिक्रिया है। आरक्षण के विरोध से उपजा आक्रोश,’’ नितिन ने वितृष्णा से भरकर कहा।
‘‘डीन ही नहीं प्रोफेसर भी इसी तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, और प्रणव मिश्रा जैसे छात्रों को शह देते हैं,’’ अमरदीप ने नितिन मेश्राम की बात का समर्थन किया।
सुभाष सोनकर अपने भीतर उठते गुस्से को दबाते हुए बोला, ‘‘मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई थी। जिसे लेकर पुलिस थाने गया था रपट लिखाने। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया था—यह तुम लोगों का अन्दरूनी मामला है। पुलिस को क्यों घसीटते हो...अब आप ही बताइए। आखिर हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। इन स्थितियों में ठीक से पढ़ाई में भी एकाग्र हो जाना मुश्किल हो जाता है।’’
रमेश चौधरी ने अखबारों को भी रपट भेजी थी जिसमें दलित छात्रों के उत्पीड़न को मुख्य मुद्दा बनाया था। लेकिन अखबारों ने इसे रैगिंग कहकर छापा। दलित छात्रों के साथ होनेवाली ज्यादतियों का कहीं जिक्र तक नहीं था।
विचार-विमर्श के बाद राकेश और रमेश चौधरी डीन से मिलकर समस्या का कोई न कोई समाधान तलाश करेंगे। जरूरत पड़ी तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलकर बात करेंगे।
मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर भगवती उपाध्याय से मिलने पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। डीन का कहना था कि आरक्षण से मेडिकल का स्तर गिर रहा है। राकेश ने उन्हें टोकते हुए कहा था, ‘‘डॉक्टर साहब, हम यहाँ आरक्षण के पक्ष या विपक्ष पर चर्चा करने नहीं दलित छात्रों की समस्याएँ लेकर आए हैं।’’
डीन उनकी कोई भी सुने बगैर आरक्षण से होनेवाले नुकसान पर ही बोल रहे थे। उनकी धारणा थी कि कम योग्यतावाले जब सरकारी हस्तक्षेप से मेडिकल जैसे संस्थानों में घुसपैठ करेंगे तो हालात तो दिन-प्रतिदिन खराब होंगे ही। उन छात्रों का क्या दोष जो अच्छे अंक लेकर पास हुए हैं।
राकेश बहस से बचना चाह रहा था, ‘‘डॉक्टर साहब, आरक्षण पर हम लोग फिर कभी चर्चा कर लेंगे, अभी तो उन हालात का कोई समाधान निकालिए, जिनकी हमने चर्चा की है। दलित छात्रों का उत्पीड़न रोकिए।’’
‘‘देखिए, छोटी-मोटी घटनाओं को इतना तूल मत दें। दलित उत्पीड़न जैसा मेरे कॉलेज में कुछ नहीं है। और मैं इन वाहियात चीजों को नहीं मानता। हमारे घर में तो भंगिन को भी ‘अम्मा’ कहा जाता था,’’ डीन जैसे अपने आप से बाहर ही नहीं निकल रहे थे।
राकेश और रमेश चौधरी बौखलाकर उठ आए थे। दलित छात्रों का मेडिकल में आना डीन की दृष्टि में घुसपैठ थी। रमेश चौधरी ने स्वयं को बहुत मुश्किल से काबू में रखा था। शायद राकेश के कारण।
कई दिन वे दोनों अनेक गण्यमान्य लोगों से मिले। लेकिन सभी जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अनेक दलित अधिकारियों के पास वे गए। उनका रवैया भी निराशाजनक ही था। वे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उनका कहना था, मामले उठाने से दलित छात्रों का नुकसान होगा।
दस-पन्द्रह दिन के अथक प्रयासों के बाद भी कोई सुगबुगाहट वे पैदा करने में असफल रहे थे। निराश होकर रमेश चौधरी ने कहा था, ‘‘राकेश साहब अब तो आपने खुद ही देख लिया...मैं इन लोगों से क्यों कड़वी बात करता हूँ....’’
राकेश भी अधिकारी था। लेकिन वह छात्रों की मदद करना चाहता था, सामाजिक उत्तरदायित्व समझकर। सरकारी अफसर ऐसे कामों से बचने की कोशिश करते थे। उन्हें डर था, कहीं इन हादसों के छीटों में वे भीग न जाएँ। उन्हें दलित होने का भय हर वक्त सालता है।
रमेश ने जुलूस निकालने की योजना बना ली थी। तारीख भी तय हो गई थी। लेकिन अचानक सुभाष सोनकर की आत्महत्या ने सबकुछ बदलकर रख दिया था। सबसे ज्यादा सदमा पहुँचा था रमेश चौधरी को। इस खबर से वह गुस्से से बिफर पड़ा था। राकेश को जब उसने सोनकर की आत्महत्या का समाचार दिया उस वक्त वह आपे से बाहर था।
सोनकर को पहली ही परीक्षा में फेल कर दिया गया था। क्योंकि उसने प्रणव मिश्रा के खिलाफ पुलिस में नामजद रपट लिखाने का दुस्साहस किया था, डीन और अन्य प्रोफेसरों तक शिकायत पहुँचाने की हिमाकत की थी, यह भूलकर कि वह इस चक्रव्यूह में अकेला फँस गया है, जहाँ से बाहर आने के लिए उसे कौरवों की कई अक्षौहिणी सेना और अनेक महारथियों से टकराना पड़ेगा। परीक्षाफल का व्यूह भेदकर सोनकर बाहर नहीं आ पाया था। कई महारथियों ने निहत्थे सोनकर की हत्या कर दी थी। जिसे आत्महत्या कहकर प्रचारित किया गया था।
रमेश चौधरी से फोन पर यह समाचार पाकर राकेश भी गहरे अवसाद से भर गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी कुशाग्र बुद्धि का सोनकर आत्महत्या कर सकता है। फोन पर रमेश की आक्रोशित आवाज सुनकर राकेश की उलझनें औऱ ज्यादा बढ़ गई थीं। उसके काँपते हाथ में थमा फोन भी थरथरा गया था। बहुत मुश्किल से राकेश फोन क्रेडिल पर रख पाया था....राकेश ने स्वयं को सँभालने का प्रयास किया। फिर भी उसे लग रहा था जैसे उसका हृदय डूब रहा है। वह धम्म से कुर्सी में धंस गया। उसके मुँह से अस्फुट शब्द निकले, ‘‘सोनकर यह क्यों किया तुमने....!’’
राकेश के मन बुरी तरह उचट गया था। दफ्तर के काम में भी मन नहीं लग रहा था। वह दफ्तर से उठकर जाने ही वाला था, फोन की घंटी बज उठी। रमेश चौधरी का फोन था। धीर-गम्भीर आवाज में बोल रहा था, ‘‘राकेश साहब, कल पोस्ट मार्टम के बाद सोनकर की लाश का अन्तिम संस्कार मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर होगा...आपमें साहस हो तो पहुँच जाना....’’
रमेश चौधरी के शब्दों में छिपी आँच को उसने महसूस कर लिया था। वह अभी तक सोनकर की मौत के सदमे से उबर नहीं पाया था कि रमेश चौधरी के इस फैसले ने उसे पेशोपेश में डाल दिया था। सोनकर का चेहरा बार-बार उसकी आँखों में उतर रहा था। राकेश अपने भीतर उठनेवाली बेचैनी को जितना दबाने की कोशिश कर रहा था, वह उतनी ही तीव्रता से बढ़ रही थी। वह फिर से कुर्सी पर बैठ गया था। सोनकर का चेहरा उसे उद्वेलित कर रहा था। सोनकर की जद्दोजहद राकेश की अपनी पीड़ा बन गई थी। उसने एक गहरी साँस ली और झटके से उठकर खड़ा हो गया था। उसने तय कर लिया था, वह सोनकर की अन्तिम यात्रा में शामिल ही नहीं होगा, उसे कन्धा भी देगा।
राकेश के दफ्तर पहुँचते ही फोन की घंटी बजी। रमेश चौधरी का फोन था। उसने काँपती आवाज में कहा था, ‘‘राकेश साहब, सुभाष सोनकर बलि चढ़ गया है...’’
‘‘क्या ?...’’ राकेश ने लगभग चीखते हुए पूछा।
‘‘अभी और कितनी हत्याएँ होंगी राकेश साहब ?...’’ रमेश ने अपनी बात जारी रखी थी, ‘‘आखिर सोनकर का अपराध क्या था ?...सिर्फ इतना की माँ-बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे।’’ रमेश चौधरी का एक-एक शब्द गहरी वेदना से बाहर आ रहा था।
राकेश काठ की तरह जड़ हो गया था। रमेश चौधरी की भर्राई आवाज जैसे हजारों मील दूर से आ रही थी। जिसे वह ठीक से सुन नहीं पा रहा था। सोनकर की मौत का राकेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था। राकेश को लग रहा था जैसे रमेश चौधरी किसी गहरी खाई में खड़ा है। जहाँ से प्रतिध्वनित होकर आ रही आवाज धीमी हो गई थी। जिसे सुन पाना राकेश के लिए कठिन महसूस हो रहा था।
सुभाष सोनकर का उदास चेहरा राकेश की आँखों के सामने बार-बार आ रहा था। उसे लगा फोन उसकी पकड़ से फिसल रहा है।
उसकी स्मृति में वह दिन दस्तक देने लगा, जब रमेश चौधरी सुभाष सोनकर और उसके मित्रों को लेकर आया था।
उस रोज वह दफ्तर से घर आते ही अखबार लेकर बैठ गया था। रसोई में इन्दु की खटर-पटर चल रही थी। बच्चे दूसरे कमरे में अपना होमवर्क कर रहे थे। घर का वातावरण शान्त था, लेकिन दफ्तर से आते ही अखबार से चिपक जाना इन्दू को चिढ़ाने के लिए काफी था। उसने व्यंग्य से पूछा, ‘‘कहीं जाना है क्या ?’’
‘‘नहीं...क्यों ?’’ राकेश हड़बड़ा गया था।
‘‘कपड़े नहीं बदले...?’’ इन्दू ने शंका जाहिर की।
राकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। दरअसल वह कुछ बेचैन था। दफ्तर में रमेश चौधरी का फोन आया था। कुछ जरूरी बात करना चाहता था। शाम को घर आएगा। राकेश ने टालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रमेश चौधरी माना ही नहीं था। राकेश ने कहा भी था, ‘‘दफ्तर में ही आ जाओ।’’ लेकिन रमेश चौधरी ने कहा था, ‘‘नहीं, बात कुछ ऐसी ही है जो दफ्तर में नहीं हो सकती है।’’
रमेश चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता है। अक्सर किसी न किसी बहाने वह राकेश के पास आता ही रहता है। जब भी वह आता है राकेश अव्यवस्थित हो उठता है। उससे जितना बचने का प्रयास करो, वह उतना ही पीछे पड़ा रहता है। रमेश चौधरी के बोलने का अन्दाज कुछ ऐसा था कि सामनेवाला व्यक्ति सहज नहीं रह पाता था।
‘‘...तुम लोग अपने आपको समझते क्या हो ? तुम लोगों को सिर्फ बड़े-बड़े प्रमोशन चाहिए, वे भी आरक्षण के भरोसे। बच्चों को स्कूल-कॉलेज में एडमीशन भी कोटे से ही चाहिए। लेकिन इस कोटे को बचाए रखने के लिए जब कुछ करने की नौबत आती है तो तुम लोगों को जरूरी काम निकल आते हैं या फिर दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती। तब रमेश चौधरी ही बनेगा बलि का बकरा। गालियाँ भी वही खाएगा। देखो साहब...अगर भीड़ का हिस्सा बनने में आप लोगों को खतरा दिखाई देता तो ऐसी संस्थाओं को चंदा दो जो तुम्हारे हितों के लिए काम करती हैं...तुम लोग इसी तरह उदासीन बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब आरक्षण को ये लोग हजम कर जाएँगे....बाबा साहब तो हैं नहीं...और बाबा साहब के नुमाइन्दे बनने का जो ढोंग कर रहे हैं वे भी संसद में पहुँचते ही गीदड़ बनकर उनकी गोद में बैठ जाते हैं जो आरक्षण विरोधी हैं, और तरह-तरह की नौटंकियाँ करने में माहिर हैं। न्यायाधीशों से फैसले दिलवाएँगे कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग में आरक्षण से दाखिला नहीं मिलेगा। इससे प्रतिभाएँ नष्ट होती हैं...जैसे प्रतिभाएँ इनकी गुलाम हैं और सिर्फ इनके घरों में ही जन्मती हैं...अरे इतने ही प्रतिभावान थे तो देश की यह हालत कैसे हो गई...’’
ऐसे संवादों से राकेश आएँ-बाएँ देखने लगता है। और यदि यह वार्तालाप घर में चल रहा होता तो इन्दु को लगता है जैसे अडो़सी-पड़ोसी कान लगाकर सुन रहे हैं। इस वार्तालाप से इन्दु ऐसी उखड़ती है कि कई-कई दिन तक घर में गोलाबारी चलती ही रहती है। ऐसे में राकेश एकतरफा युद्धधविराम घोषित करके आत्मसमर्पण की मुद्रा अख्तियार कर लेता है।
इन्दु घुमा-फिराकर यही कहती है :
‘‘...तुम चाहे जितने बड़े अफसर बन जाओ, मेल-जोल इन लोगों से ही रखोगे, जिन्हें यह तमीज भी नहीं है कि सोफे पर बैठा कैसे जाता है...तुम्हें इनसे यारी-दोस्ती करना है तो घर से बाहर ही रखो...आस पड़ोस में जो थोड़ी-बहुत इज्जत है, उसे भी क्यों खत्म करने पर तुले हो...गले में ढोल बाँधकर मत घूमो...यह जो सरनेम लगा रखा है...यही क्या कम है...कितनी बार कहा है कि इसे बदलकर कुछ अच्छा-सा सरनेम लगाओ...बच्चे बड़े हो रहे हैं...इन्हें कितना सहना पड़ता है। कल पिंकी की सहेली कह रही थी...रैदास तो जूते बनाता था...तुम लोग भी जूते बनाते हो...पिंकी रोते हुए घर आई थी...मेरा तो जी करता है बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊँ...’’ इन्दु की यह तानाकशी राकेश को बौना बना देती है। वह खुद अपराध बोध से भर जाता है।
बस अखबार खोलकर बैठ जाता है। ऐसे अखबार की सुर्खियाँ गड्डमड्ड होकर काले धब्बों में बदल जाती हैं। और राकेश को लगने लगता है जैसे वह सुरक्षित है।
दरवाजे की घंटी बजने से उसकी विचार तन्द्रा टूट गई थी। उसने दरवाजा खोला। रमेश चौधरी ही था। उसके साथ चार युवा और थे। वे सब अन्दर आकर इधर-उधर पसर गए थे। राकेश उन्हें गौर से देख रहा था। सभी के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उदास चेहरों पर भय की परछाइयाँ दिखाई पड़ रही थीं।
वे सभी चुप थे। सभी अपने-अपने खोल में सिमटे हुए थे। खोल से बाहर आने की छटपटाहट उनके चेहरों से ज्यादा उनकी आँखों में थी। उनकी दशा देखकर राकेश के मन में कई तरह की शंकाएँ पनपने लगी थीं।
रमेश चौधरी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ‘‘राकेश साहब, यह है अमरदीप, ये विकास चौधरी, ये नितिन मेश्राम और ये सुभाष सोनकर। सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। अमरदीप और नितिन मेश्राम फाइनल वर्ष में हैं और ये दोनों प्रथम वर्ष में हैं। आपसे मिलना चाहते थे।’’
‘‘हाँ...जरूर...’’राकेश ने सहज भाव से कहा।
अमरदीप हिचकते हुए बोला, ‘‘सर ! हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं...समझ नहीं आ रहा है क्या करें ?’’ अमरदीप पल-भर के लिए रुका। खुद को व्यवस्थित करते हुए बोला, ‘‘मेडिकल कॉलेज के जो हालात हैं, उसमें हमारे लिए पढ़ाई जारी रखना दिन-प्रतिदिन कठिन हो रहा है। ये साल हमने जिन यातनाओं के साथ गुजारे हैं...हम ही जानते हैं। कई बार तो लगता था पढ़ाई छोड़कर वापस लौट जाएँ...लेकिन माँ-बाप की उम्मीदें रास्ता रोककर मजबूर कर देती हैं। उन सब यातनाओं के साथ पढ़ाई जारी रखना...बहुत तकलीफदेह है...एक रोज तो मैंने आत्महत्या तक करने का निश्चय कर लिया था।’’ निराशा और हताशा से लबरेज अमरदीप के शब्दों ने साँझ के धुँधलकों को और अधिक गहरा दिया था। अमरदीप के अन्तस से गूँजती चीत्कारें साफ-साफ सुनाई पड़ रही थीं।
माहौल गमगीन हो गया था। राकेश के हृदय में जैसे कम्पन बढ़ गए थे। अपने ही अन्तर्मन की हिलोरों पर तैरता अमरदीप बोला, ‘‘कल पूरा दिन होस्टल के एक कमरे में विकास चौधरी और सुभाष सोनकर को दरवाजा बन्द करके पीटा गया।’’
‘‘क्यों...? क्या रैगिंग चल रही थी ?’’ राकेश ने हैरानी से पूछा।
‘रैगिंग होती तो फर्स्टइयर के सभी छात्रों के साथ यह सुलूक होता। लेकिन वहाँ तो सिर्फ इन दोनों को ही पीटा गया,’’ अमरदीप ने जोर देकर कहा।
‘दलित छात्रों को अलग खड़ा करके अपमानित करना तो रोज का किस्सा है। प्रवेश परीक्षा के प्रतिशत अंक पूछकर थप्पड़ या घूँसों से प्रहार होता है। जरा भी विरोध किया तो लात पड़ती है। यह दो-चार दिन नहीं साल के साल चलता है। और यह पिटाई कॉलेज या छात्रावास तक ही सीमित नहीं है। शहर से कॉलेज तक जानेवाली बस में भी पिटाई होती है। कोई एक सीनियर चलती बस में चिल्लाकर कहता है, ‘‘इस बस में जो भी चमार स्टूडैंट है...वह खड़ा हो जाए...फिर उसे धकियाकर पिछली सीटों पर ले जाया जाता, जहाँ पहले से बैठे सीनियर लात, घूँसो से उसका स्वागत करते हैं।’’ अमरदीप ने हालात का ब्यौरा दिया।
‘‘यह तो सरासर जुल्म है,’’ राकेश ने उत्तेजित होते हुए कहा। अमरदीप ने राकेश की ओर देखा,...‘‘अभी कुछ दिन पहले ऐसी ही बस में फाइनल के प्रणव मिश्रा ने चिल्लाकर अवाज लगाई तो उस बस में सुभाष सोनकर था, जो प्रणव की आवाज पर चुपचाप रहा। सोनकर के पास जो छात्र बैठा था, उसने इशारे से बता दिया कि सोनकर यहाँ बैठा है। प्रणव मिश्रा अपनी अवहेलना पर तिलमिला गया। सोनकर के बाल पकड़कर अपनी ओर खींचे, ‘क्यों बे चमरटे सुनाई नहीं पड़ा हमने क्या कहा था ?’ सोनकर ने अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की...मैं चमार नहीं हूँ। बालों की पकड़ मजबूत थी। सोनकर कराह उठा। प्रणव मिश्रा का झन्नाटेदार थप्पड़ सोनकर के गाल पर पड़ा...(गाली)...चमार हो या सोनकर...ब्राह्मण तो नहीं हो...हो तो सिर्फ कोटेवाले...बस इतना ही काफी है, प्रणव मिश्रा ने सोनकर को लात-घूँसों से अधमरा कर दिया। पूरी बस में ठहाके गूँज रहे थे...बाबा साहब के नाम पर गालियाँ दी जा रही थीं। प्रणव मिश्रा के इस शौर्य पर उसे शाबाशियाँ मिल रही थीं।’’
राकेश ने सोनकर की ओर देखा। वह अपराधी की मुद्रा में सिर झुकाए बैठा था। सोनकर के चेहरे पर चोट के निशान और गहरे हो गए थे।
रमेश चौधरी भी खामोश था। लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियाँ कसी हुई थीं। चेहरे का रंग बदल रहा था। रसोई में इन्दु की खटर-पटर और तेज हो गई थी। इन्दु के खँखारने का स्वर राकेश के लिए संकेत था....‘अजी, आप इन पचड़ों में न पड़ो।’ रसोई के कामकाज के दौरान भी इन्दु के कान इन लोगों की बातचीत पर ही लगे थे।
इन्दु का जो नजरिया था, वह सामाजिक प्रताणना का प्रतिफल था। वह एक सहज जीवन जीना चाहती थी। उसे लगता था राकेश को इन झमेलों से बचना चाहिए। वह इसी कोशिश में लगी रहती थी कि आस-पड़ोस के लोग उनके बारे में न जान पाएँ कि वे कौन हैं ? उसे यह सब बहुत सुरक्षित लगता था। लेकिन राकेश उनकी व्यथा-कथा से विचलित हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि वे सब किसी घने बियाबान जंगल में फँस गए हैं जहाँ चारों ओर सिर्फ अँधेरा है या कँटीले झाड़-झंखाड़।
इन्दु रसोईं से निकलकर बेडरूम में चली गई थी। जहाँ बच्चे अपने होमवर्क में मशगूल थे। कुछ ही क्षण बाद राकेश का आठ वर्षीय पुत्र बाहर आया। आदेशात्मक लहजे में राकेश से बोला, ‘‘पापा ! मेरा होमवर्क कराओ।’’
‘‘हाँ, बेटे, बस अभी कराते हैं, दस मिनट में....जरा रमेश अंकल से बात कर लें...तब तक तुम अपनी ड्राइंग बना लो,’’ राकेश ने उसे बहला-फुसलाकर वापस भेज दिया। राकेश इन्दु का इशारा समझ रहा था—‘इन्हें जल्दी भगाओ...इन झंझटों से अपने आपको दूर रखो।’
राकेश कुछ अटपटा-सा गया था। रमेश चौधरी ने भी इशारा समझ लिया था। वह सहज बने रहना चाहता था। उसने राकेश को धीरे से कहा, ‘‘साहब, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे...बस इन लड़कों को कोई रास्ता सुझाइए....डॉक्टर तो इन्हें बनना ही है....।’’
राकेश गहरी सोच में था। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि इन हालात में छात्रों को क्या करना चाहिए।
नितिन मेश्राम अभी तक चुप था। राकेश को गहरी सोच में डूबा देखकर बोला, ‘‘होस्टल नं. एक में कमरा एलॉट हो जाने के बाद किसी दलित छात्र को उसमें घुसने नहीं दिया जाता है। घूम-फिरकर होस्टल नं. दो में ही दलित छात्रों को रखा जाता है। यही स्थिति गर्ल्स होस्टल की भी है। वहाँ की सभी दलित लड़कियाँ एक ही होस्टल में रहती हैं। कॉलेज मैनेजमेंट को ये समस्याएँ गंभीर नहीं लगतीं। उन्हें लगता है दलितों के लिए मेडिकल में आना अतिक्रमण करना है। जब उनसे शिकायत करते हैं तो ध्यान ही नहीं देते।’’
नितिन मेश्राम मुखर हो उठा था, ‘‘इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में भी भेदभाव बरता जाता है। प्रणव मिश्रा मेरे ही बैच में है। न क्लासेज अटेंड करता है, न प्रैक्टिकल। फिर भी त्रिवेदी सर उसे ही सबसे ज्यादा अंक देते हैं। अटैंडेंस की भी समस्या नहीं होती।’’ मेश्राम ने कटुता से कहा।
राकेश की स्मृतियों में अतीत दस्तक देने लगा था। जब वह पहली बार होस्टल गया था। उसे जो रूम एलॉट हुआ था उसमें पहले से एक छात्र था जिसने उसे अपने कमरे में घुसने ही नहीं दिया था। उसने साफ मना कर दिया था कि वह किसी भंगी-चमार के साथ अपना रूम शेयर नहीं कर सकता है। जब उसने होस्टल वार्डन से शिकायत की तो उसने भी उसकी जाति पूछी थी और उसे एक दलित छात्र के साथ रख दिया था। साथ ही उसे चेतावनी भी दी थी—‘अपनी औकात में रहो...वरना बाहर कर दूँगा।’
छात्रावास जीवन के दिन बहुत ही पीड़ादायक थे। एक-एक दिन जैसे यन्त्रणा से गुजर कर पार करना पड़ता था। मैस में भी अलग बैठना पड़ता था।
रमेश चौधरी ने राकेश की सोच को झटका दिया, ‘‘साहब, अब आप ही बताइए क्या किया जाए ?’’
‘‘तुम लोग डीन से मिले ?’’ राकेश ने सवाल किया।
‘‘जी, मिले थे...उनका कहना है—आरक्षण से आए हो थोड़ा-बहुत तो सहना ही होगा। सवर्ण छात्रों की ज्यादतियों को वे अनुचित नहीं मानते। क्योंकि नाइंसाफी के खिलाफ ये प्रतिक्रिया है। आरक्षण के विरोध से उपजा आक्रोश,’’ नितिन ने वितृष्णा से भरकर कहा।
‘‘डीन ही नहीं प्रोफेसर भी इसी तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, और प्रणव मिश्रा जैसे छात्रों को शह देते हैं,’’ अमरदीप ने नितिन मेश्राम की बात का समर्थन किया।
सुभाष सोनकर अपने भीतर उठते गुस्से को दबाते हुए बोला, ‘‘मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई थी। जिसे लेकर पुलिस थाने गया था रपट लिखाने। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया था—यह तुम लोगों का अन्दरूनी मामला है। पुलिस को क्यों घसीटते हो...अब आप ही बताइए। आखिर हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। इन स्थितियों में ठीक से पढ़ाई में भी एकाग्र हो जाना मुश्किल हो जाता है।’’
रमेश चौधरी ने अखबारों को भी रपट भेजी थी जिसमें दलित छात्रों के उत्पीड़न को मुख्य मुद्दा बनाया था। लेकिन अखबारों ने इसे रैगिंग कहकर छापा। दलित छात्रों के साथ होनेवाली ज्यादतियों का कहीं जिक्र तक नहीं था।
विचार-विमर्श के बाद राकेश और रमेश चौधरी डीन से मिलकर समस्या का कोई न कोई समाधान तलाश करेंगे। जरूरत पड़ी तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलकर बात करेंगे।
मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर भगवती उपाध्याय से मिलने पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। डीन का कहना था कि आरक्षण से मेडिकल का स्तर गिर रहा है। राकेश ने उन्हें टोकते हुए कहा था, ‘‘डॉक्टर साहब, हम यहाँ आरक्षण के पक्ष या विपक्ष पर चर्चा करने नहीं दलित छात्रों की समस्याएँ लेकर आए हैं।’’
डीन उनकी कोई भी सुने बगैर आरक्षण से होनेवाले नुकसान पर ही बोल रहे थे। उनकी धारणा थी कि कम योग्यतावाले जब सरकारी हस्तक्षेप से मेडिकल जैसे संस्थानों में घुसपैठ करेंगे तो हालात तो दिन-प्रतिदिन खराब होंगे ही। उन छात्रों का क्या दोष जो अच्छे अंक लेकर पास हुए हैं।
राकेश बहस से बचना चाह रहा था, ‘‘डॉक्टर साहब, आरक्षण पर हम लोग फिर कभी चर्चा कर लेंगे, अभी तो उन हालात का कोई समाधान निकालिए, जिनकी हमने चर्चा की है। दलित छात्रों का उत्पीड़न रोकिए।’’
‘‘देखिए, छोटी-मोटी घटनाओं को इतना तूल मत दें। दलित उत्पीड़न जैसा मेरे कॉलेज में कुछ नहीं है। और मैं इन वाहियात चीजों को नहीं मानता। हमारे घर में तो भंगिन को भी ‘अम्मा’ कहा जाता था,’’ डीन जैसे अपने आप से बाहर ही नहीं निकल रहे थे।
राकेश और रमेश चौधरी बौखलाकर उठ आए थे। दलित छात्रों का मेडिकल में आना डीन की दृष्टि में घुसपैठ थी। रमेश चौधरी ने स्वयं को बहुत मुश्किल से काबू में रखा था। शायद राकेश के कारण।
कई दिन वे दोनों अनेक गण्यमान्य लोगों से मिले। लेकिन सभी जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अनेक दलित अधिकारियों के पास वे गए। उनका रवैया भी निराशाजनक ही था। वे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उनका कहना था, मामले उठाने से दलित छात्रों का नुकसान होगा।
दस-पन्द्रह दिन के अथक प्रयासों के बाद भी कोई सुगबुगाहट वे पैदा करने में असफल रहे थे। निराश होकर रमेश चौधरी ने कहा था, ‘‘राकेश साहब अब तो आपने खुद ही देख लिया...मैं इन लोगों से क्यों कड़वी बात करता हूँ....’’
राकेश भी अधिकारी था। लेकिन वह छात्रों की मदद करना चाहता था, सामाजिक उत्तरदायित्व समझकर। सरकारी अफसर ऐसे कामों से बचने की कोशिश करते थे। उन्हें डर था, कहीं इन हादसों के छीटों में वे भीग न जाएँ। उन्हें दलित होने का भय हर वक्त सालता है।
रमेश ने जुलूस निकालने की योजना बना ली थी। तारीख भी तय हो गई थी। लेकिन अचानक सुभाष सोनकर की आत्महत्या ने सबकुछ बदलकर रख दिया था। सबसे ज्यादा सदमा पहुँचा था रमेश चौधरी को। इस खबर से वह गुस्से से बिफर पड़ा था। राकेश को जब उसने सोनकर की आत्महत्या का समाचार दिया उस वक्त वह आपे से बाहर था।
सोनकर को पहली ही परीक्षा में फेल कर दिया गया था। क्योंकि उसने प्रणव मिश्रा के खिलाफ पुलिस में नामजद रपट लिखाने का दुस्साहस किया था, डीन और अन्य प्रोफेसरों तक शिकायत पहुँचाने की हिमाकत की थी, यह भूलकर कि वह इस चक्रव्यूह में अकेला फँस गया है, जहाँ से बाहर आने के लिए उसे कौरवों की कई अक्षौहिणी सेना और अनेक महारथियों से टकराना पड़ेगा। परीक्षाफल का व्यूह भेदकर सोनकर बाहर नहीं आ पाया था। कई महारथियों ने निहत्थे सोनकर की हत्या कर दी थी। जिसे आत्महत्या कहकर प्रचारित किया गया था।
रमेश चौधरी से फोन पर यह समाचार पाकर राकेश भी गहरे अवसाद से भर गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी कुशाग्र बुद्धि का सोनकर आत्महत्या कर सकता है। फोन पर रमेश की आक्रोशित आवाज सुनकर राकेश की उलझनें औऱ ज्यादा बढ़ गई थीं। उसके काँपते हाथ में थमा फोन भी थरथरा गया था। बहुत मुश्किल से राकेश फोन क्रेडिल पर रख पाया था....राकेश ने स्वयं को सँभालने का प्रयास किया। फिर भी उसे लग रहा था जैसे उसका हृदय डूब रहा है। वह धम्म से कुर्सी में धंस गया। उसके मुँह से अस्फुट शब्द निकले, ‘‘सोनकर यह क्यों किया तुमने....!’’
राकेश के मन बुरी तरह उचट गया था। दफ्तर के काम में भी मन नहीं लग रहा था। वह दफ्तर से उठकर जाने ही वाला था, फोन की घंटी बज उठी। रमेश चौधरी का फोन था। धीर-गम्भीर आवाज में बोल रहा था, ‘‘राकेश साहब, कल पोस्ट मार्टम के बाद सोनकर की लाश का अन्तिम संस्कार मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर होगा...आपमें साहस हो तो पहुँच जाना....’’
रमेश चौधरी के शब्दों में छिपी आँच को उसने महसूस कर लिया था। वह अभी तक सोनकर की मौत के सदमे से उबर नहीं पाया था कि रमेश चौधरी के इस फैसले ने उसे पेशोपेश में डाल दिया था। सोनकर का चेहरा बार-बार उसकी आँखों में उतर रहा था। राकेश अपने भीतर उठनेवाली बेचैनी को जितना दबाने की कोशिश कर रहा था, वह उतनी ही तीव्रता से बढ़ रही थी। वह फिर से कुर्सी पर बैठ गया था। सोनकर का चेहरा उसे उद्वेलित कर रहा था। सोनकर की जद्दोजहद राकेश की अपनी पीड़ा बन गई थी। उसने एक गहरी साँस ली और झटके से उठकर खड़ा हो गया था। उसने तय कर लिया था, वह सोनकर की अन्तिम यात्रा में शामिल ही नहीं होगा, उसे कन्धा भी देगा।
हंस, मई, 2000
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book