|
कहानी संग्रह >> भस्मावृत चिनगारी भस्मावृत चिनगारीयशपाल
|
50 पाठक हैं |
||||||
नैतिक और सामाजिक दायित्वों पर आधारित कहानियाँ...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
हमारे पूर्वज साहित्य की दृष्टि से वंश उत्पत्ति के स्रोत नारी की शुद्धता
सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु थी। वह दृष्टिकोण और प्रयोजन नैतिक था, यह हम
स्वीकार करते हैं परन्तु आज के लेखक का भी प्रयोजन हो सकता है-वह चाहता है
हमारे समाज का आधा भाग नारी समाज भी आज के कठिन संघर्ष में अपने आर्थिक,
राजनैतिक और सामाजिक दायित्व को समझे और वह केवल पुरुष के कन्धों पर बोझ
ही न बनी रहे।
कला और साहित्य का उद्देश्य सभी अवस्थाओं में मनुष्य की नैतिकता और कर्तव्य की प्रवृत्तियों की चिनगरियों को भावना की फूँक मार कर सुलगाना ही रहता है। अन्तर रहता है, हमारे विश्वास और दृष्टिकोण में। कभी हम समझते हैं इन चिनगारियों में से निकली ज्वाला प्रकाश का मार्ग दिखाएगी, कभी हम समझते है हैं कि यह ज्वाला हमारे समाज की रक्षा करने वाले छप्पर को फूँक कर राख कर देगी।
हिन्दी कहानी की विकास परम्परा में यशपाल अकेले लेखक हैं, जिनमें यथार्थवादी रचनादृष्टि के अनेक रुप विद्यामान हैं। कथा-वस्तु ही नहीं, शिल्प के स्तर पर भी उनका अवदान हिन्दी कहानी में ऐसा है जिसे रेखांकित किया जाना बाकी है। परम्परागत कथा-रुप से लेकर आख्यान के शिल्प तक उनके प्रयोगों का विस्तार है। कथा-वस्तु के क्षेत्र में कल्पना से लेकर वस्तुगत यथार्थ और फिर सामाजिक यथार्थ की सहज भूमि पर उतर कर अन्वेषण और उद्घाटन तक उनका कथा-सृजन फैला हुआ है। इस तरह देखें तो वे हिन्दी कहानी के एक मात्र स्रष्टा हैं उन्होंने प्रसूत, भावात्मक सृजन से शुरू करके कथा वाचन तक की लम्बी कथा-यात्रा इन कहानियों में पूरी की है। आख्यातिक के शिल्प तक पहुँचते-पहुँचते यशपाल कहानी को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानने लगते है।
1939 से 1979 के बीच प्रकाशित सत्रह कथा-संकलनों में फैला हुआ उनका विशाल कहानी लेखन हिन्दी साहित्य की गौरवपूर्ण उपलब्धि है जिसे अब लोकभारती चार भागों में प्रकाशित कर ऐसे पाठक वर्ग तथा पुस्तकालयों की माँग को पूरा कर रहा है जो एक लम्बे अरसे से यशपाल की कहानियों के ग्रंथावली-रूप की माँग कर रहा था।
परिवर्तन के इस युग में हमारे प्रतिष्ठित साहित्यिक और कलाकार सतर्क और चिन्तित हैं। उन्हें भय या, उत्साह और उत्तेजना से मूढ़ नयी पीढ़ी के साहित्यकों और कलाकारों के हाथ में पड़ कर हमारी परम्परागत कला अपनी शुद्धता, प्रतिभा और प्रयोजन न खो बैठे। नयी पीढ़ी के कलाकार कला के सभी रूपों, कविता, कहानी और चित्रकला का उपयोग, अपनी सूझ के अनुसार वर्तमान समस्याओं की अभिव्यक्ति और उनके हल के लिए निर्ममता और निरंकुशता से कर रहे हैं। प्रतिष्ठित कलाकारों की आशंका एक सीमा तक युक्तिसंगत है। उत्तेजना मूढ़ता और निरंकुशता से सभी वस्तुओं और साधनों का अनियमित प्रयोग भोंड़ा और बेढंगा हो सकता है। प्रश्न यही है कि नयी पीढ़ी के कलाकार मूढ़ और निरंकुश है या नहीं ?
कला मनुष्य के सभी भावों का परिमार्जित रूप है। ऐसा रूप जो कलाकार-व्यक्ति समाज के विचार चिंतन और उपयोग के लिए समाज के सम्मुख प्रस्तुत करता है। स्थान और समय के भेद से जैसे मनुष्य के विचारों को प्रकट करने का मुख्य साधन भाषा पृथक- पृथक होती है वैसे ही स्थान और समय के अन्तर के भावों अथवा कला के प्रकट करने के साधनों या बाहरी रूप में अन्तर आ जाना आवश्यक है। स्थान और समय का दूसरा नाम है परिस्थितियाँ। परिस्थितियों से न केवल भाव को प्रकट करने वाले साधनों के रूप में अन्तर आ जाता है बल्कि भाव भी दूसरे प्रकार के हो जा सकते हैं। मनुष्य के भाव या भावना की परिभाषा की जाय तो हम उसे संक्षेप में मनुष्य की महत्त्वाकांक्षा कह सकते हैं। एक छोटी मछली की महत्त्वाकांक्षा हाथी बनने की होगी- मगरमच्छ बनने की कल्पना शायद चींटी न कर सके।
मनुष्य की परिस्थितियों का प्रभाव न केवल कला की उत्पत्ति और रूप पर पड़ता है बल्कि कला के मूल्यांकन पर भी पड़ता है। कला का कौन रूप और कौन सीमा कुरुचिपूर्ण, वासनात्मक और प्रचारात्मक हो जाती यह बात आलोचक और समाज के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है- जैसे सभी मनुष्यों के लिए पथ्य एक ही वस्तुएं नहीं हो सकती। वैसे नग्नता के बारे में हमारा संस्कार और अभ्यास उचित-अनुचित का निश्चय करते हैं, वैसे ही वासना के संबंध में भी। किसी स्थान और समय में मुँह ढाँक कर पेट उघाड़ा रखना लज्जाशीलता हो सकता है, दूसरे समय और स्थान में इससे ठीक उलटे।
हमारे चरित्रवान पूर्वजों के सुसंस्कृत साहित्य में नारी को ‘मोहिनी’ ‘सुमुखी’ और ‘नितम्बिनी’ संबोधन करना शालीनता थी। आज हमारे हीन चरित्र समाज में किसी स्त्री को उसके मुख पर ‘सुन्दरी’ कहना जूतों की मार को निमंत्रण देना है। महाकवि कालिदास का नारी की रोमांचित जंघा का वर्णन करना, हर और सती की रतिक्रिया का चित्रण न अश्लील समझा गया न वासनात्मक परन्तु यदि आज का लेखक नारी के वस्त्रों के भीतर दृष्टि मात्र पहुँचाने का प्रयत्न करता है तो भी वह नैतिकता का शत्रु समझा जाता है। इस पर हमें संताप यह है कि हम नैतिकता की दृष्टि से पूर्वजों की अपेक्षा बहुत गिरते जा रहे है। संभवत: कारण यह है कि वासना को चरितार्थ करने की क्षमता हममें अपने पूर्वजों के समान नहीं रह गयी है। मन्दाग्नि के रोगी के समान घी हमारे लिए विष हो गया है। सदाचार और नैतिकता का एक दृष्टिकोण और मानदण्ड हमारे पूर्वजों के सामने भी था और एक हमारे सामने भी है।
इसी प्रकार प्रचार भी समस्या है। कलाकार के भाव और कल्पना जीवन के अनुभवों की भूमि पर ही खड़े हो सकते हैं। यदि कला जीवन की समस्या का आना दोष है तो फिर कला का प्रत्यक्ष रूप है क्या ? किसी भी कलाकार की कृति जीवन का एक रूप में पाये बिना प्रकट नहीं हो सकती। प्रश्न है- कला में प्रकट जीवन का रूप किस समस्या का संदेश देता है ? भावशून्य, संदेशशून्य कला को क्या हम कला कह सकते हैं ? यहाँ भी निर्णय का आधार हमारे संस्कार और अभ्यास ही हैं। जिन भावों और सन्देशों को हम परम्परा और अभ्यास से स्वीकार करते आये हैं, कला में उनकी समावेश हमें केवल शाश्वत सत्य की प्रतिष्ठा जान पड़ता है, प्रचार नहीं। स्वामी की सेवा में सेवक के जान पर खेल जाने का करुण चित्रण हमारी कलात्मक वृत्तियों को गुमशुदा कर सद्वृत्तियों को जगाने वाला समझा जाता है। वह हमें प्रचार नहीं जान पड़ता। दुश्चरित्र पति की निन्दा न सुनने के लिए पतिव्रता के कान मूँद लेने की कहानी में केवल आदर्श जीवन की प्रतिष्ठा ही जान पड़ती है, प्रचार नहीं।
परन्तु जब आज का कलाकार अन्नदाता स्वामी के लिए सेवक के प्राण-त्याग की भावना को विद्रूप कर उसकी उपमा कुत्ते से देता है तो यह न्याय और कुतर्क जान पड़ता है। इसी प्रकार जब आज की कहानी लेखक मध्यम श्रेणी की एक सम्मानित महिला और वेश्या में यही अन्तर होता है कि सम्मानित महिला का पालन केवल एक व्यक्ति करता है और वेश्या का पालन अनेक व्यक्ति करते हैं, तब आज के लेखक पर घोर अनाचार का दोष लगाया जाता है।
हमारे पूर्वज साहित्यिक की दृष्टि में वंश उत्पत्ति के स्रोत्र नारी की शुद्घता सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु थी। वह दृष्टिकोण और प्रयोजन नैतिक था, यह हम स्वीकार करते हैं परन्तु आज के लेखक का भी प्रयोजन हो सकता है – वह चाहता है हमारे समाज का आधा भाग नारी समाज भी आज के कठिन संघर्ष में अपने आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक दायित्व को समझे और वह केवल पुरुष के कन्धों पर बोझ ही न बनी रहे।
कला और साहित्य का उद्देश्य सभी अवस्थाओं में मनुष्य में नैतिकता और कर्तव्य की प्रवृत्तियों की चिनगारियों को भावना की फूँक मार कर सुलगाना ही रहता है। अन्तर रहता है, हमारे विश्वास और दृष्टिकोण में। कभी हम समझते हैं इन चिनगारियों से निकली ज्वाला प्रकाश कर मार्ग दिखाएगी, कभी हम समझते कि यह ज्वाला हमारे समाज की रक्षा करने वाले छप्पर को फूँक कर राख कर देगी।
कला और साहित्य का उद्देश्य सभी अवस्थाओं में मनुष्य की नैतिकता और कर्तव्य की प्रवृत्तियों की चिनगरियों को भावना की फूँक मार कर सुलगाना ही रहता है। अन्तर रहता है, हमारे विश्वास और दृष्टिकोण में। कभी हम समझते हैं इन चिनगारियों में से निकली ज्वाला प्रकाश का मार्ग दिखाएगी, कभी हम समझते है हैं कि यह ज्वाला हमारे समाज की रक्षा करने वाले छप्पर को फूँक कर राख कर देगी।
हिन्दी कहानी की विकास परम्परा में यशपाल अकेले लेखक हैं, जिनमें यथार्थवादी रचनादृष्टि के अनेक रुप विद्यामान हैं। कथा-वस्तु ही नहीं, शिल्प के स्तर पर भी उनका अवदान हिन्दी कहानी में ऐसा है जिसे रेखांकित किया जाना बाकी है। परम्परागत कथा-रुप से लेकर आख्यान के शिल्प तक उनके प्रयोगों का विस्तार है। कथा-वस्तु के क्षेत्र में कल्पना से लेकर वस्तुगत यथार्थ और फिर सामाजिक यथार्थ की सहज भूमि पर उतर कर अन्वेषण और उद्घाटन तक उनका कथा-सृजन फैला हुआ है। इस तरह देखें तो वे हिन्दी कहानी के एक मात्र स्रष्टा हैं उन्होंने प्रसूत, भावात्मक सृजन से शुरू करके कथा वाचन तक की लम्बी कथा-यात्रा इन कहानियों में पूरी की है। आख्यातिक के शिल्प तक पहुँचते-पहुँचते यशपाल कहानी को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानने लगते है।
1939 से 1979 के बीच प्रकाशित सत्रह कथा-संकलनों में फैला हुआ उनका विशाल कहानी लेखन हिन्दी साहित्य की गौरवपूर्ण उपलब्धि है जिसे अब लोकभारती चार भागों में प्रकाशित कर ऐसे पाठक वर्ग तथा पुस्तकालयों की माँग को पूरा कर रहा है जो एक लम्बे अरसे से यशपाल की कहानियों के ग्रंथावली-रूप की माँग कर रहा था।
परिवर्तन के इस युग में हमारे प्रतिष्ठित साहित्यिक और कलाकार सतर्क और चिन्तित हैं। उन्हें भय या, उत्साह और उत्तेजना से मूढ़ नयी पीढ़ी के साहित्यकों और कलाकारों के हाथ में पड़ कर हमारी परम्परागत कला अपनी शुद्धता, प्रतिभा और प्रयोजन न खो बैठे। नयी पीढ़ी के कलाकार कला के सभी रूपों, कविता, कहानी और चित्रकला का उपयोग, अपनी सूझ के अनुसार वर्तमान समस्याओं की अभिव्यक्ति और उनके हल के लिए निर्ममता और निरंकुशता से कर रहे हैं। प्रतिष्ठित कलाकारों की आशंका एक सीमा तक युक्तिसंगत है। उत्तेजना मूढ़ता और निरंकुशता से सभी वस्तुओं और साधनों का अनियमित प्रयोग भोंड़ा और बेढंगा हो सकता है। प्रश्न यही है कि नयी पीढ़ी के कलाकार मूढ़ और निरंकुश है या नहीं ?
कला मनुष्य के सभी भावों का परिमार्जित रूप है। ऐसा रूप जो कलाकार-व्यक्ति समाज के विचार चिंतन और उपयोग के लिए समाज के सम्मुख प्रस्तुत करता है। स्थान और समय के भेद से जैसे मनुष्य के विचारों को प्रकट करने का मुख्य साधन भाषा पृथक- पृथक होती है वैसे ही स्थान और समय के अन्तर के भावों अथवा कला के प्रकट करने के साधनों या बाहरी रूप में अन्तर आ जाना आवश्यक है। स्थान और समय का दूसरा नाम है परिस्थितियाँ। परिस्थितियों से न केवल भाव को प्रकट करने वाले साधनों के रूप में अन्तर आ जाता है बल्कि भाव भी दूसरे प्रकार के हो जा सकते हैं। मनुष्य के भाव या भावना की परिभाषा की जाय तो हम उसे संक्षेप में मनुष्य की महत्त्वाकांक्षा कह सकते हैं। एक छोटी मछली की महत्त्वाकांक्षा हाथी बनने की होगी- मगरमच्छ बनने की कल्पना शायद चींटी न कर सके।
मनुष्य की परिस्थितियों का प्रभाव न केवल कला की उत्पत्ति और रूप पर पड़ता है बल्कि कला के मूल्यांकन पर भी पड़ता है। कला का कौन रूप और कौन सीमा कुरुचिपूर्ण, वासनात्मक और प्रचारात्मक हो जाती यह बात आलोचक और समाज के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है- जैसे सभी मनुष्यों के लिए पथ्य एक ही वस्तुएं नहीं हो सकती। वैसे नग्नता के बारे में हमारा संस्कार और अभ्यास उचित-अनुचित का निश्चय करते हैं, वैसे ही वासना के संबंध में भी। किसी स्थान और समय में मुँह ढाँक कर पेट उघाड़ा रखना लज्जाशीलता हो सकता है, दूसरे समय और स्थान में इससे ठीक उलटे।
हमारे चरित्रवान पूर्वजों के सुसंस्कृत साहित्य में नारी को ‘मोहिनी’ ‘सुमुखी’ और ‘नितम्बिनी’ संबोधन करना शालीनता थी। आज हमारे हीन चरित्र समाज में किसी स्त्री को उसके मुख पर ‘सुन्दरी’ कहना जूतों की मार को निमंत्रण देना है। महाकवि कालिदास का नारी की रोमांचित जंघा का वर्णन करना, हर और सती की रतिक्रिया का चित्रण न अश्लील समझा गया न वासनात्मक परन्तु यदि आज का लेखक नारी के वस्त्रों के भीतर दृष्टि मात्र पहुँचाने का प्रयत्न करता है तो भी वह नैतिकता का शत्रु समझा जाता है। इस पर हमें संताप यह है कि हम नैतिकता की दृष्टि से पूर्वजों की अपेक्षा बहुत गिरते जा रहे है। संभवत: कारण यह है कि वासना को चरितार्थ करने की क्षमता हममें अपने पूर्वजों के समान नहीं रह गयी है। मन्दाग्नि के रोगी के समान घी हमारे लिए विष हो गया है। सदाचार और नैतिकता का एक दृष्टिकोण और मानदण्ड हमारे पूर्वजों के सामने भी था और एक हमारे सामने भी है।
इसी प्रकार प्रचार भी समस्या है। कलाकार के भाव और कल्पना जीवन के अनुभवों की भूमि पर ही खड़े हो सकते हैं। यदि कला जीवन की समस्या का आना दोष है तो फिर कला का प्रत्यक्ष रूप है क्या ? किसी भी कलाकार की कृति जीवन का एक रूप में पाये बिना प्रकट नहीं हो सकती। प्रश्न है- कला में प्रकट जीवन का रूप किस समस्या का संदेश देता है ? भावशून्य, संदेशशून्य कला को क्या हम कला कह सकते हैं ? यहाँ भी निर्णय का आधार हमारे संस्कार और अभ्यास ही हैं। जिन भावों और सन्देशों को हम परम्परा और अभ्यास से स्वीकार करते आये हैं, कला में उनकी समावेश हमें केवल शाश्वत सत्य की प्रतिष्ठा जान पड़ता है, प्रचार नहीं। स्वामी की सेवा में सेवक के जान पर खेल जाने का करुण चित्रण हमारी कलात्मक वृत्तियों को गुमशुदा कर सद्वृत्तियों को जगाने वाला समझा जाता है। वह हमें प्रचार नहीं जान पड़ता। दुश्चरित्र पति की निन्दा न सुनने के लिए पतिव्रता के कान मूँद लेने की कहानी में केवल आदर्श जीवन की प्रतिष्ठा ही जान पड़ती है, प्रचार नहीं।
परन्तु जब आज का कलाकार अन्नदाता स्वामी के लिए सेवक के प्राण-त्याग की भावना को विद्रूप कर उसकी उपमा कुत्ते से देता है तो यह न्याय और कुतर्क जान पड़ता है। इसी प्रकार जब आज की कहानी लेखक मध्यम श्रेणी की एक सम्मानित महिला और वेश्या में यही अन्तर होता है कि सम्मानित महिला का पालन केवल एक व्यक्ति करता है और वेश्या का पालन अनेक व्यक्ति करते हैं, तब आज के लेखक पर घोर अनाचार का दोष लगाया जाता है।
हमारे पूर्वज साहित्यिक की दृष्टि में वंश उत्पत्ति के स्रोत्र नारी की शुद्घता सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु थी। वह दृष्टिकोण और प्रयोजन नैतिक था, यह हम स्वीकार करते हैं परन्तु आज के लेखक का भी प्रयोजन हो सकता है – वह चाहता है हमारे समाज का आधा भाग नारी समाज भी आज के कठिन संघर्ष में अपने आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक दायित्व को समझे और वह केवल पुरुष के कन्धों पर बोझ ही न बनी रहे।
कला और साहित्य का उद्देश्य सभी अवस्थाओं में मनुष्य में नैतिकता और कर्तव्य की प्रवृत्तियों की चिनगारियों को भावना की फूँक मार कर सुलगाना ही रहता है। अन्तर रहता है, हमारे विश्वास और दृष्टिकोण में। कभी हम समझते हैं इन चिनगारियों से निकली ज्वाला प्रकाश कर मार्ग दिखाएगी, कभी हम समझते कि यह ज्वाला हमारे समाज की रक्षा करने वाले छप्पर को फूँक कर राख कर देगी।
भस्मावृत्त चिनगारी
वह मेरे पड़ोस में रहता था। उसके प्रति मुझे एक प्रकार की श्रद्धा थी।
उसका व्यवहार एक रहस्य के कोहरे से घिरा था। रहस्य बनावट का नहीं जो
आशंकित कर देता है; सरलता का रहस्य, जो आकर्षण और सहानुभूति पैदा करता है।
वह साधारण से भिन्न था, शायद साधारण से कुछ ऊँचा।
उसके बड़े और छोटे भाइयों ने अपने श्रम से पिता की कमाई सम्पत्ति की बुनियाद पर स्वतंत्र कारोबार की इमारतें सफलतापूर्वक खड़ी कर ली थीं। वे सफल गृहस्थ और सम्मानित नागरिक बन गये थे। वे पुराने परिवार-वृक्ष की कलमों के रूप में नयी भूमि पा, नये परिवारों की लहलहाती शाखाओं के रूप में कल्ला उठे थे। पिता को अपने दोनों पुत्रों की सफलता पर गर्व और संतोष था।
और ‘वह’ सब सुविधा और अवसर होने पर और अपने शैथिल्य के कारण पिता की अधिक करणा पाकर भी कुछ न बन सका। उसने यत्न ही नहीं किया। उसके पिता को इससे उदासी और निरुत्साह हुआ; परन्तु मैं उसका आदर करता था। उसमें लोभ न था। वह संतोष की मूर्ति था। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा उसमें न थी। यही तो तपस्या है।
पिता की मृत्यु के बाद दोनों कर्मठ व्यापारी भाईयों ने हजारों की आमदनी होते हुए जब उत्तराधिकार की सम्पत्ति के बँटवारे में पाई-पाई का हिसाब कर, उसे केवल दो पुराने मकान देकर ही निबटा दिया; उसने कोई चिन्ता या व्यग्रता प्रकट न की। भाइयों की अपने से दस-बीस गुना अधिक आमदनी के प्रति उसे कभी ईर्ष्या करते नहीं देखा। घर में अर्थ-संकट अनुभव करके भी उसे कभी विचलित होते नहीं देखा। उसकी शान्त और सौंदर्य की वृत्ति सभी जगह शान्ति और सौंदर्य पा सकती थी। इनका स्रोत्र उसके भीतर था। वह अन्तर्मुख और आत्मरत था। कला के लिए उसका जीवन था और कला ही उसके प्राण थी। कला से किसी प्रकार की स्वार्थ साधना उसे कला का अपमान जान पड़ता था।
उसके परिचय का क्षेत्र अधिक विस्तृत न था। परिचय से उसे घबराहट होती थी। उसके चित्रों से प्रभावित होकर मैंने स्वयं ही उससे परिचय किया था। वह कुछ सकुचाया और फिर जैसे उसने मुझे सह लिया और आन्तरिकता भी बढ़ती गयी। कभी वह संध्या, दोपहर या बिलकुल तड़के ही आ बैठता। उसका समय कोई निश्चित न था। कभी अकेले ही शहर से चार-पाँच मील दूर जाकर बैठा रहता। उसका सब समय प्राय: किर्मिच मढ़ी टिकटी के आस-पास रंग-घुली प्यालियों और कूचियों के चक्कर में बीत जाता था।
वह बहुत कम बोलता था। जब बोलता उसमें बहुत-सी विचित्र बातें रहती थीं। सहमत हुए बिना भी उनकी कद्र करनी पड़ती थी। क्योंकि वह एक असाधारण व्यक्ति की बातें थीं। सूख कर ऐंठ गये पत्तों और सूर्य की किरणों में मकड़ी के जाले पर झलमलाती ओस की बूँदों में उसे जाने क्या-क्या दीखता था ?........वह उनमें खो जाता था।
एक दिन मई महीने में ठीक दोपहर के समय मोटर में छावनी से लौट रहा था। सूर्य की किरणों से वाष्प बन रही धूल में, बियावान सड़क पर उसे अकेले शहर की ओर लौटते देखा। उसके समीप गाड़ी रोक कर पुकारा- ‘‘इस समय कहाँ ?’’
‘‘ऐसे ही जरा घूमने निकला था।’’ उत्तर मिला।
विस्मयाहत होकर पूछा, ‘‘इस धूप में ?’’ कार का दरवाजा उसके लिए खोलकर आग्रह किया, ‘‘आओ !’’
‘‘नहीं, तुम चलो !’’ अपनी धोती का छोर थामे, मेरे विस्मय की ओर ध्यान दिये बिना उसने उत्तर दिया।
एक तरह से जबरन ही उसे गाड़ी में बैठा लिया। मजबूरी की हालत में मेरे समीप कुछ क्षण चुपचाप बैठकर उसने धीमे से कहा- ‘‘देखो कितना सुन्दर है........जैसे पालिश की हुई चाँदी फैल गयी हो ! जैसे........बर्फ पड़ जाने के बाद उसका गुण बदल गया हो......... White heat (श्वेत उत्ताप) और देखो, तरल गरमी की लपटें कैसे पृथ्वी से आकाश की ओर उड़ी जा रही है। मेरी ओर दृष्टि कर उसने कहा- ‘‘जरा यह काला चश्मा उतार कर देखो !’’
मजबूरन चश्मा उतारना पड़ा। आँखों में जैसे तीर से चुभ गये। और फिर जो उसने कहा था ठीक भी जँचने लगा। सोचा, कितना असाधारण है यह व्यक्ति ? यह शायद संसार के लिए एक विभूति है।
ऐसे ही एक दूसरे दिन शरद ऋतु की संध्या के समय बड़े पार्क के किनारे वृक्षों के नीचे से, सूखी घास पर गिरे सूखे, कुड़मुड़ाये पत्तों को रौंदते धोती को छोर थामे, अपना फटा पम्प शू रगड़ते उसे उतावली में चले जाते देखा।
पुकारा। उसने सुना नहीं।
अगले दिन उसके यहाँ जाकर देखा, वह तन्मय किर्मिच-मढ़ी के सामने खड़ा कूची से रंग लगा रहा है। बहुत ही सुन्दर चित्र था- हाल में अस्त हुए सूर्य की गहरी, सिन्दूरी आभा आकाश में अर्धवृत्ताकार फैल रही थी। उस पृष्ठभूमि पर आकाश की ओर उठी हुई उँगली की तरह एक सूखे पेड़ की टहनी पर श्याम चिरैया का जोड़ा प्रणयाकुल हो रहा था।
विस्मय-मुग्ध नेत्रों से कुछ देर तक चित्र को देखकर उससे पूछा- ‘‘कल तुम पार्क के समीप से जा रहे थे, पुकारा तो तुमने सुना ही नहीं।’’
प्रश्नात्मक दृष्टि से उसने मेरी ओर देखा, कुछ सोचकर उत्तर दिया- ‘‘कल पार्क में चिड़िया के जोड़े को इस प्रकार देखा और वह तुरन्त ही उड़ गया.........। सोचा इस चीज को यदि स्थायी रूप दे सकूँ.........।’’
उसके अनेक चित्रों ‘निर्वासन’, ‘गौरीशंकर’, ‘गंगा और सागर’ ने प्रसिद्धि नहीं पायी परन्तु विश्वास से कह सकता हूँ, जिस दिन पारखी आँखें उन चित्रों को देख पाएँगी, संसार चकित रह जाएगा। मुझे गर्व था ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार की मैत्री का।
मेरा विचार था, वह सांसारिकता से तटस्थ है; भावुकता के साम्राज्य में ही वह रहता है। परन्तु एक दिन हम उसी के मकान पर बैठे थे। वह न जाने किस विचार में खो गया। उस चुप से उकता कर भी विघ्न न डाला। सोचा, न जाने किस अमूल्य कृति के अंकुर इसके मस्तिष्क में जन्म पा रहे हों ?
समीप के जीने पर उसकी साढ़े तीन बरस की लड़की खेल रही थी। वह अलापने लगी- ‘पापा........पापा.......पापा !’ मानों नींद से जाग कर उसने कहा, ‘how sweet- कितना मधुर........?’ समझा कलाकार भी मनुष्य होता है।
लक्ष्मी के लिए विद्वानों ने चपला शब्द ठीक ही प्रयोग किया है। वह स्थिर नहीं रहती। कलाकार के एक मकान में भूतों ने डेरा डाल दिया और उसका किराये पर उठना कठिन हो गया। उसकी आमदनी कम होती थी। अच्छे-भले मध्यम श्रेणी के खाते-पीते आदमी से उसकी हालत खस्ता हो गयी परन्तु उस ओर उसका ध्यान न गया। उपाय सुझाने और स्वयं उपाय कर देने के लिए तैयार होने पर भी उसने इस बात को महत्त्व न दिया। उसे इससे कोई मतलब न था। त्याग और तपस्या क्या दूसरी चीज होती है ?
दूसरे बालक के प्रसव से पहले उसकी स्त्री बीमार हो गयी। वह बीमारी असाधारण थी। खर्च भी असाधारण था। दो महीने में साढ़े तीन हजार रुपया खर्च हो गया। एक मकान पहले से गिरवी था, दूसरा भी गया। कोई शिकायत उसे न थी। उसने केवल इतना कहा- ‘‘यदि रुपये से मनुष्य के प्राण बच सकते हैं तो वह किसी भी मूल्य पर महँगा नहीं। किसी तरह स्त्री के प्राण बचे।
उसके बड़े और छोटे भाइयों ने अपने श्रम से पिता की कमाई सम्पत्ति की बुनियाद पर स्वतंत्र कारोबार की इमारतें सफलतापूर्वक खड़ी कर ली थीं। वे सफल गृहस्थ और सम्मानित नागरिक बन गये थे। वे पुराने परिवार-वृक्ष की कलमों के रूप में नयी भूमि पा, नये परिवारों की लहलहाती शाखाओं के रूप में कल्ला उठे थे। पिता को अपने दोनों पुत्रों की सफलता पर गर्व और संतोष था।
और ‘वह’ सब सुविधा और अवसर होने पर और अपने शैथिल्य के कारण पिता की अधिक करणा पाकर भी कुछ न बन सका। उसने यत्न ही नहीं किया। उसके पिता को इससे उदासी और निरुत्साह हुआ; परन्तु मैं उसका आदर करता था। उसमें लोभ न था। वह संतोष की मूर्ति था। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा उसमें न थी। यही तो तपस्या है।
पिता की मृत्यु के बाद दोनों कर्मठ व्यापारी भाईयों ने हजारों की आमदनी होते हुए जब उत्तराधिकार की सम्पत्ति के बँटवारे में पाई-पाई का हिसाब कर, उसे केवल दो पुराने मकान देकर ही निबटा दिया; उसने कोई चिन्ता या व्यग्रता प्रकट न की। भाइयों की अपने से दस-बीस गुना अधिक आमदनी के प्रति उसे कभी ईर्ष्या करते नहीं देखा। घर में अर्थ-संकट अनुभव करके भी उसे कभी विचलित होते नहीं देखा। उसकी शान्त और सौंदर्य की वृत्ति सभी जगह शान्ति और सौंदर्य पा सकती थी। इनका स्रोत्र उसके भीतर था। वह अन्तर्मुख और आत्मरत था। कला के लिए उसका जीवन था और कला ही उसके प्राण थी। कला से किसी प्रकार की स्वार्थ साधना उसे कला का अपमान जान पड़ता था।
उसके परिचय का क्षेत्र अधिक विस्तृत न था। परिचय से उसे घबराहट होती थी। उसके चित्रों से प्रभावित होकर मैंने स्वयं ही उससे परिचय किया था। वह कुछ सकुचाया और फिर जैसे उसने मुझे सह लिया और आन्तरिकता भी बढ़ती गयी। कभी वह संध्या, दोपहर या बिलकुल तड़के ही आ बैठता। उसका समय कोई निश्चित न था। कभी अकेले ही शहर से चार-पाँच मील दूर जाकर बैठा रहता। उसका सब समय प्राय: किर्मिच मढ़ी टिकटी के आस-पास रंग-घुली प्यालियों और कूचियों के चक्कर में बीत जाता था।
वह बहुत कम बोलता था। जब बोलता उसमें बहुत-सी विचित्र बातें रहती थीं। सहमत हुए बिना भी उनकी कद्र करनी पड़ती थी। क्योंकि वह एक असाधारण व्यक्ति की बातें थीं। सूख कर ऐंठ गये पत्तों और सूर्य की किरणों में मकड़ी के जाले पर झलमलाती ओस की बूँदों में उसे जाने क्या-क्या दीखता था ?........वह उनमें खो जाता था।
एक दिन मई महीने में ठीक दोपहर के समय मोटर में छावनी से लौट रहा था। सूर्य की किरणों से वाष्प बन रही धूल में, बियावान सड़क पर उसे अकेले शहर की ओर लौटते देखा। उसके समीप गाड़ी रोक कर पुकारा- ‘‘इस समय कहाँ ?’’
‘‘ऐसे ही जरा घूमने निकला था।’’ उत्तर मिला।
विस्मयाहत होकर पूछा, ‘‘इस धूप में ?’’ कार का दरवाजा उसके लिए खोलकर आग्रह किया, ‘‘आओ !’’
‘‘नहीं, तुम चलो !’’ अपनी धोती का छोर थामे, मेरे विस्मय की ओर ध्यान दिये बिना उसने उत्तर दिया।
एक तरह से जबरन ही उसे गाड़ी में बैठा लिया। मजबूरी की हालत में मेरे समीप कुछ क्षण चुपचाप बैठकर उसने धीमे से कहा- ‘‘देखो कितना सुन्दर है........जैसे पालिश की हुई चाँदी फैल गयी हो ! जैसे........बर्फ पड़ जाने के बाद उसका गुण बदल गया हो......... White heat (श्वेत उत्ताप) और देखो, तरल गरमी की लपटें कैसे पृथ्वी से आकाश की ओर उड़ी जा रही है। मेरी ओर दृष्टि कर उसने कहा- ‘‘जरा यह काला चश्मा उतार कर देखो !’’
मजबूरन चश्मा उतारना पड़ा। आँखों में जैसे तीर से चुभ गये। और फिर जो उसने कहा था ठीक भी जँचने लगा। सोचा, कितना असाधारण है यह व्यक्ति ? यह शायद संसार के लिए एक विभूति है।
ऐसे ही एक दूसरे दिन शरद ऋतु की संध्या के समय बड़े पार्क के किनारे वृक्षों के नीचे से, सूखी घास पर गिरे सूखे, कुड़मुड़ाये पत्तों को रौंदते धोती को छोर थामे, अपना फटा पम्प शू रगड़ते उसे उतावली में चले जाते देखा।
पुकारा। उसने सुना नहीं।
अगले दिन उसके यहाँ जाकर देखा, वह तन्मय किर्मिच-मढ़ी के सामने खड़ा कूची से रंग लगा रहा है। बहुत ही सुन्दर चित्र था- हाल में अस्त हुए सूर्य की गहरी, सिन्दूरी आभा आकाश में अर्धवृत्ताकार फैल रही थी। उस पृष्ठभूमि पर आकाश की ओर उठी हुई उँगली की तरह एक सूखे पेड़ की टहनी पर श्याम चिरैया का जोड़ा प्रणयाकुल हो रहा था।
विस्मय-मुग्ध नेत्रों से कुछ देर तक चित्र को देखकर उससे पूछा- ‘‘कल तुम पार्क के समीप से जा रहे थे, पुकारा तो तुमने सुना ही नहीं।’’
प्रश्नात्मक दृष्टि से उसने मेरी ओर देखा, कुछ सोचकर उत्तर दिया- ‘‘कल पार्क में चिड़िया के जोड़े को इस प्रकार देखा और वह तुरन्त ही उड़ गया.........। सोचा इस चीज को यदि स्थायी रूप दे सकूँ.........।’’
उसके अनेक चित्रों ‘निर्वासन’, ‘गौरीशंकर’, ‘गंगा और सागर’ ने प्रसिद्धि नहीं पायी परन्तु विश्वास से कह सकता हूँ, जिस दिन पारखी आँखें उन चित्रों को देख पाएँगी, संसार चकित रह जाएगा। मुझे गर्व था ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार की मैत्री का।
मेरा विचार था, वह सांसारिकता से तटस्थ है; भावुकता के साम्राज्य में ही वह रहता है। परन्तु एक दिन हम उसी के मकान पर बैठे थे। वह न जाने किस विचार में खो गया। उस चुप से उकता कर भी विघ्न न डाला। सोचा, न जाने किस अमूल्य कृति के अंकुर इसके मस्तिष्क में जन्म पा रहे हों ?
समीप के जीने पर उसकी साढ़े तीन बरस की लड़की खेल रही थी। वह अलापने लगी- ‘पापा........पापा.......पापा !’ मानों नींद से जाग कर उसने कहा, ‘how sweet- कितना मधुर........?’ समझा कलाकार भी मनुष्य होता है।
लक्ष्मी के लिए विद्वानों ने चपला शब्द ठीक ही प्रयोग किया है। वह स्थिर नहीं रहती। कलाकार के एक मकान में भूतों ने डेरा डाल दिया और उसका किराये पर उठना कठिन हो गया। उसकी आमदनी कम होती थी। अच्छे-भले मध्यम श्रेणी के खाते-पीते आदमी से उसकी हालत खस्ता हो गयी परन्तु उस ओर उसका ध्यान न गया। उपाय सुझाने और स्वयं उपाय कर देने के लिए तैयार होने पर भी उसने इस बात को महत्त्व न दिया। उसे इससे कोई मतलब न था। त्याग और तपस्या क्या दूसरी चीज होती है ?
दूसरे बालक के प्रसव से पहले उसकी स्त्री बीमार हो गयी। वह बीमारी असाधारण थी। खर्च भी असाधारण था। दो महीने में साढ़े तीन हजार रुपया खर्च हो गया। एक मकान पहले से गिरवी था, दूसरा भी गया। कोई शिकायत उसे न थी। उसने केवल इतना कहा- ‘‘यदि रुपये से मनुष्य के प्राण बच सकते हैं तो वह किसी भी मूल्य पर महँगा नहीं। किसी तरह स्त्री के प्राण बचे।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book









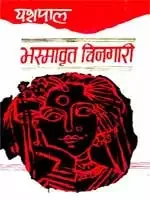


_s.webp)
