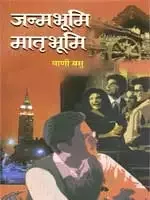|
प्रवासी >> जन्मभूमि मातृभूमि जन्मभूमि मातृभूमिवाणी बसु
|
107 पाठक हैं |
||||||
यह पुस्तक अपने देश को छोड़कर विदेश में जा बसे उन लोगों के लिए है जिनके परिजन आज भी अपने देश में ही हैं
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
बँगला में सुविख्यात यह उपन्यास उन लोगों की व्यथा-कथा है, जिनकी जन्मभूमि
तो विदेशी है, लेकिन मातृभूमि भारत है। वहाँ जनमे बच्चों की समस्याएँ कुछ
अलग हैं। अपनी जड़ो से उखड़कर विदेश में जा बसे बच्चों के सामने एक ओर तो
विदेशों का स्थूल आकर्षक, वहाँ का वातावरण, वहाँ की संस्कृति व परंपराएँ
उनपर अपना प्रभाव डाल रही हैं, दूसरी ओर उन्हें अपने माता-पिता से यह
शिक्षा मिलती है कि उनका देश भारत है। वहाँ की संस्कृति ही उनकी अपनी
संस्कृति है।
अमेरिका और भारत-दोनों देशों की पृष्ठभूमि समेटे इस उपन्यास के सभी चरित्र बेहद सजीव और वास्तविक लगते हैं।
विभिन्न मानवीय संबंधों की उलझनों की विश्लेषण। मानव चरित्र के उन तंतुओं पर प्रकाश, उन पर करारा आघात, जो जिंदगी के ताने-बाने को जटिल बनाते हैं। अत्यंत रोचक एवं पठनीय उपन्यास।
अमेरिका और भारत-दोनों देशों की पृष्ठभूमि समेटे इस उपन्यास के सभी चरित्र बेहद सजीव और वास्तविक लगते हैं।
विभिन्न मानवीय संबंधों की उलझनों की विश्लेषण। मानव चरित्र के उन तंतुओं पर प्रकाश, उन पर करारा आघात, जो जिंदगी के ताने-बाने को जटिल बनाते हैं। अत्यंत रोचक एवं पठनीय उपन्यास।
सार संक्षेप
‘जन्मभूमि-मातृभूमि’ उपन्यास में विदेशों में जा बसे
भारतीयों की समस्या खासकर उनकी उत्तरपीढ़ी की समस्या का रोचक और मार्मिक
विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह उन लोगों की व्यथा-कथा है, जिनकी जन्मभूमि
तो विदेश है, लेकिन मातृभूमि भारत। इसमें वहाँ जन्मे भारतीय बच्चों की
समस्याएँ, असमंजस, अवधाराणाएँ और मोहबंध का जीवंत विवरण है। अपनी जड़ों से
उखड़कर विदेश में जा बसे बच्चों के सामने एक ओर विदेशों का स्थूल आकर्षण
वहाँ का माहौल, वहाँ की संस्कृति-परंपराएँ उनपर अपना असर डाल रही हैं,
दूसरी ओर उन्हें अपने माता-पिता से यह शिक्षा मिलती है कि उनका देश भारत
है, वहाँ की संस्कृति ही उनकी अपनी है। जिन बातों और आचरणों को वे नितांत
सहज और स्वाभाविक मानते हैं, अपने माता-पिता की तरफ से उनका विरोध पाकर वे बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं। उच्च महत्त्वाकांक्षाएँ दौलत की चाह, बेहतर
सुख-सुविधाएँ और अच्छी सी नौकरी की चाह भारतीयों को विदेश की ओर खींच तो
ले जाती है, मगर उनके बच्चे, अपने इर्द-गिर्द के माहौल के अनुसार विदेशी
संस्कृति की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो उन्हें अपनी मातृभूमि, अपनी भारतीय
संस्कृति याद आने लगती है। इसके अलावा, अपने प्रति विदेशों का भेदभावपूर्ण
बरताव भी उनका मोहभंग करता है। अंदर-ही-अंदर वे लोग नितांत अकेलेपन के
शिकार हो जाते हैं। वे लोग विदेश में भी अपने देश की मिट्टी, अपनी
संस्कृति को थामे रखने की कोशिश करते हैं और महसूस करते हैं कि प्रवास
उन्हें निपट अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं देगा। जब उन्हें अपनी भूल का अहसास
होता है, तो वे अपने परिवार समेत स्वदेश लौट जाते हैं।
लेकिन अब, भारत क्या वही भारत है ? स्वदेश में फैली दुर्नीति, अकर्मण्यता राजनीतिक भ्रष्टाचार गुटबाजी बढ़ती हुई अनुशासनहीनता इत्यादि उन लोगों को अजीब पसोपेश में डाल देते हैं। लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति उनका प्यार भले सबकुछ मान लेने को विवश करे, लेकिन उनके बच्चे इसे स्वीकार नहीं कर पाते। सुदीप और कमलिका का बेटा, चूँकि इसी देश में पैदा हुआ है, अपनी दादी और अन्यान्य परिवारीजनों से जुड़ा हुआ है, वह इन स्थितियों को स्वीकार कर लेता है। मगर विदेश में जनमी बेटी मणि भारत आकर घोर असमंजस में पड़ जाती है। वह देखती है कि जिन विकृतियों ने अमेरिका को अपने शिकंजे में कस रखा है उन सबने भारतीयों को भी घेर लिया है। यहाँ गरीब लोग फुटपाथों पर दम तोड़ने को मजबूर हैं, औरतों की निर्मम हत्या की जाती है; इस देश के नौजवान अमेरिकन से बढ़कर अमेरिकन बन गए हैं। अमेरिका में बसा छोटा सा भारतीय समूह एक अविकृत भारत को अपने मन में सँजोए रखने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ के लोग पूरे जी-जान से यह भूलने की कोशिश में जुटे हैं कि वे लोग भारतीय हैं, उनकी भाषा भारतीय है। स्वदेश लौटकर मणि आस-पास का परिवेश देखकर अपनी विदेशी वेशभूषा बदल लेती है। मगर वह गौर करती है कि इस देश के लोगों का पोशाक-पहनावा खयाल धारणा, बातचीत जीवन-शैली सब पूरी तरह अमेरिकी रंग में रँग चुके हैं।
विदेशी माहौल में पली-बढ़ी मणि अपने इरादों पर दृढ़ रहती है, मगर वह गौर करती है कि यहाँ की नौजवान पीढ़ी गुमराह है। फिर भी वह तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। अच्छे परचे करने के बावजूद कम नंबर मिलते हैं। पता चलता कि बंडल-के-बंडल उत्तर कॉपियाँ अधिकारियों के यहाँ से गुम हो गई थीं और परचून की दुकान पर लिफाफा बन गईं थीं। उसकी उत्तर पुस्तिका भी उन्हीं में शामिल थी। इधर भ्रष्टाचार, गुटबाजी और छात्रों की निरंकुशता खत्म करने की कोशिश में सुदीप जब कदम उठाते हैं, तो छात्रों के पंडे उनका घेराव करते हैं, बुरी तरह अपमानित करते हैं। उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और वे दम तोड़ देते हैं। मणि महसूस करती है कि यह उसका देश नहीं है। वह इस मातृभूमि का मोह त्यागकर अपनी जन्मभूमि अमेरिका जाने का फैसला करती है।
उपन्यास में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के अहसास, अनुभव कहीं एकतरफा न हों, विदुषी लेखिका ने इस ओर भी पैनी नजर रखी है। अमेरिका और भारत-दोनों देशों की पृष्ठभूमि समेटे उपन्यास के सभी चरित्र बेहद सजीव और वास्तविक लगते हैं और पूरी कहानी ही लक्ष्यभेदी और हृदयस्पर्शी हो उठी है।
लेकिन अब, भारत क्या वही भारत है ? स्वदेश में फैली दुर्नीति, अकर्मण्यता राजनीतिक भ्रष्टाचार गुटबाजी बढ़ती हुई अनुशासनहीनता इत्यादि उन लोगों को अजीब पसोपेश में डाल देते हैं। लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति उनका प्यार भले सबकुछ मान लेने को विवश करे, लेकिन उनके बच्चे इसे स्वीकार नहीं कर पाते। सुदीप और कमलिका का बेटा, चूँकि इसी देश में पैदा हुआ है, अपनी दादी और अन्यान्य परिवारीजनों से जुड़ा हुआ है, वह इन स्थितियों को स्वीकार कर लेता है। मगर विदेश में जनमी बेटी मणि भारत आकर घोर असमंजस में पड़ जाती है। वह देखती है कि जिन विकृतियों ने अमेरिका को अपने शिकंजे में कस रखा है उन सबने भारतीयों को भी घेर लिया है। यहाँ गरीब लोग फुटपाथों पर दम तोड़ने को मजबूर हैं, औरतों की निर्मम हत्या की जाती है; इस देश के नौजवान अमेरिकन से बढ़कर अमेरिकन बन गए हैं। अमेरिका में बसा छोटा सा भारतीय समूह एक अविकृत भारत को अपने मन में सँजोए रखने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ के लोग पूरे जी-जान से यह भूलने की कोशिश में जुटे हैं कि वे लोग भारतीय हैं, उनकी भाषा भारतीय है। स्वदेश लौटकर मणि आस-पास का परिवेश देखकर अपनी विदेशी वेशभूषा बदल लेती है। मगर वह गौर करती है कि इस देश के लोगों का पोशाक-पहनावा खयाल धारणा, बातचीत जीवन-शैली सब पूरी तरह अमेरिकी रंग में रँग चुके हैं।
विदेशी माहौल में पली-बढ़ी मणि अपने इरादों पर दृढ़ रहती है, मगर वह गौर करती है कि यहाँ की नौजवान पीढ़ी गुमराह है। फिर भी वह तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। अच्छे परचे करने के बावजूद कम नंबर मिलते हैं। पता चलता कि बंडल-के-बंडल उत्तर कॉपियाँ अधिकारियों के यहाँ से गुम हो गई थीं और परचून की दुकान पर लिफाफा बन गईं थीं। उसकी उत्तर पुस्तिका भी उन्हीं में शामिल थी। इधर भ्रष्टाचार, गुटबाजी और छात्रों की निरंकुशता खत्म करने की कोशिश में सुदीप जब कदम उठाते हैं, तो छात्रों के पंडे उनका घेराव करते हैं, बुरी तरह अपमानित करते हैं। उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और वे दम तोड़ देते हैं। मणि महसूस करती है कि यह उसका देश नहीं है। वह इस मातृभूमि का मोह त्यागकर अपनी जन्मभूमि अमेरिका जाने का फैसला करती है।
उपन्यास में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के अहसास, अनुभव कहीं एकतरफा न हों, विदुषी लेखिका ने इस ओर भी पैनी नजर रखी है। अमेरिका और भारत-दोनों देशों की पृष्ठभूमि समेटे उपन्यास के सभी चरित्र बेहद सजीव और वास्तविक लगते हैं और पूरी कहानी ही लक्ष्यभेदी और हृदयस्पर्शी हो उठी है।
आत्म-स्वीकार
ऐसा ही होता है। यही वास्तविकता है। कभी रोटी-रोजगार पाने की लाचारी में,
कभी महत्त्वाकांक्षाओं की दौड़ में शामिल ज्यादातर लोग अपना देश छोड़कर
विदेशों की राह लेते हैं। परदेस में अपने देश की यादों से घिरे अपनी
संस्कृति और मान्यताओं को अपने मन में सँजोए जीते रहते हैं और किसी दिन
स्वदेश लौट आने के सपने देखते रहते हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब देश की
धरती पर जनमे उनके अपने बच्चे उस देश की संस्कृति और मान्याताओं को अपनाने लगते हैं। अपने बच्चों में भी अपनी संस्कृति की खुशबू भरने के इरादे से वे
स्वदेश लौटते हैं। मगर देश अब बदल चुका है सभ्यता जर्जर है और मान्यताएँ
जख्मी हैं। वर्तमान समय अव्यवस्था, अन्याय घोर भ्रष्टाचार और
किन्हीं-किन्हीं मामलों में बर्बरता का रूप धर चुका है, जो निहायत
निर्ममता से आदर्शों और उन आदर्शों को थामे इनसानों की जान ले लेता है।
विदेशों में जनमे बच्चे घोर असमंजस झेलते हुए फिर विदेश लौट जाने का फैसला
करते हैं। यह वापसी उदास भले हो, मगर हकीकत है। अस्तु सारा-का-सारा कसूर
क्या वर्तमान पीढ़ी के नौजवानों का है ? विदेश को ही अपना देश मान
लेनेवाले, वर्तमान पीढ़ी के बच्चे ही क्या गुनहगार हैं ? हमारे देश की
अव्यवस्था, अन्याय और भ्रष्टाचार क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं ? यहाँ
अपनी जड़ों से प्यार करने वाले शहीद हो जाते हैं या वापस लौट जाते हैं। यह
समस्या हमारी समूची व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाती है; हमसे गहरी सोच और
चिंतन की माँग करती है।
अब तक लगभग 120 बँगला उपन्यासों का अनुवाद, तीन कविता-संग्रह-अक्स-दर-अक्स’, ‘शब्द साक्षी है’, ‘आह से गुजरते हुए’ प्रकाशित। ‘सफर-सफर धूप’ प्रकाशनाधीन।
अब तक लगभग 120 बँगला उपन्यासों का अनुवाद, तीन कविता-संग्रह-अक्स-दर-अक्स’, ‘शब्द साक्षी है’, ‘आह से गुजरते हुए’ प्रकाशित। ‘सफर-सफर धूप’ प्रकाशनाधीन।
-सुशील गुप्ता
जन्मभूमि-मातृभूमि
एक
मार्च की दस तारीख हो गई, लेकिन अभी भी दो-एक दिन के अंतराल में ब्रुकलिन
का आसमान लगातार बर्फ बरसा रहा है। हमारे पंद्रह जाड़ों में तेरह जाड़े
दक्षिण में गुजरे हैं। चूँकि वह हिस्सा कर्क रेखा के काफी करीब है, इसलिए
वहाँ की आबोहवा काफी नम्र है। सिर्फ जाड़ा ही जरा कड़क है-दिल्ली की ठंड
की तरह। वह ठंड भी जनवरी के बाद से ही अपना बोरिया-बिस्तर समेटने लगती है।
इतना तुषार या ब्लिजार्ड की हमें आदत नहीं होती। मेरी राय में तो
वृष्टिपात की तरह तुषारपात को भी काँच के पार से ही देखने में मजा आता है।
इस मौसम में बाहर निकल लेना ही बेहतर है। पिछले साल, मैं जाड़े के मौसम
में ऑस्ट्रेलिया भाग खड़ा हुआ था। अकेला ही। सात हफ्तों के लिए लेक्चर
टूर। इस बहाने दक्षिण-पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कई स्थलों की सैर भी कर आया और
उत्तरी संयुक्त राज्य के जाड़े की मार से भी बच गया। सच तो यह है कि मैं
हमेशा से ही ठंड-कातर रहा हूँ। लेकिन मेरी पत्नी कमलिका-को गरमी बरदाश्त
नहीं होती ह्यूस्टन की गरमी तो कभी-कभी उष्ण कटिबंधीय गरमी के करीब-करीब
पहुँच जाती है यानी शिद्दत की गरमी पड़ती है। उसपर से गॉल्फ ऑफ मेक्सिको
की ओर से हरहराकर आती हुई तीखे दाँत-नाखूनोंवाली आँधी-झंझा ! ह्यूस्टन से
न्यूयॉर्क ! शुरू-शुरू के झोंक में यह बदली हुई आबोहवा बुरी भी नहीं लगती
थी। मेरा मित्र ज्योति हमेशा से ही यहाँ का बाशिंदा है। ब्रॅन्क्स के
अस्पताल का व्यस्त डॉक्टर ! उसने आश्वासन दिया था कि वसंत ऋतु के मध्य और
अंत के दौरान मौसम काफी सुहावना हो जाएगा। शहर की उत्तरी-दक्षिणी वीथियों
में ड्राइव करना भी बड़ा भला लगेगा।
ब्रुकलिन का मिजाज क्या इस बार बदल गया ? मुझे तो यह छलनामयी यहूदी ललना नजर आई, जिसने अपने को रहस्य के अवगुंठन में आवृत कर रखा हो। यहाँ ठंड के साथ-साथ हवा भी निहायत बेतरतीब और मस्तमौला है ! सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस ठंड के दौरान ही, कोई-कोई बेहद गुनगुना-सुनहरा दिन भी निकल आता है, फ्रेश फ्रॉम द ओवन-बेक्ड चिंगड़ी मछली की तरह। उस दिन तो अपने बदन से लंबा कोट, दस्ताने मफलर वगैरह उतार फेंकने पड़ते हैं। छुट्टी कहाँ होती है ? मगर छुट्टी का मूड बन जाता है। मेरा मन होता है कि मैं सभी लोगों को आवाज देकर पुकारूँ-‘चलो, आज स्कूल-विस्कूल, ऑफिस दफ्तर नहीं, आज हम सब हाइवे से होकर, बफैलो की तरह दौड़ जाएँ। सड़क के दोनों तरफ, उजले-धुले, ठेठ शहर-दर-शहर; वाटर-पेंटिंग जैसे गंज-कस्बे, गाँव-देहात नजर आएँगे। कुछ-कुछ दूरी पर स्थित मोटलों में कुछेक पल गुजारकर सुबह-सुबह किसी फास्ट फूड ज्वॉएंट में मोटे-मोटे हैंबर्गर और शाम को तीन-चार कोर्स इस्पहानी डिनर खाकर, हम अपनी-अपनी गुफा में लौट आएँगे।’’ लेकिन ये सब खामखयाली बातें यहाँ वीक-एंड के अलावा और किसी वक्त जुबान पर नहीं लाई जा सकतीं। इस महादेश में वह भाषा ही अचल है। लेकिन ऐसे बँधे-बँधाए नियमों के मुताबिक धूमधाम से वीक एंड मनाना मुझे सख्त नापसंद है। अरे, ऐसी जोर-जबरदस्ती की जाए तो आराम भला आराम रह पाता है ?
मैंने गौर किया है कि उत्तर की सर्दी का मौसम मेरे खत्री दोस्त वर्मन की पत्नी के हाथों तैयार किए गए दही-बड़े की तरह भारी-भरकम और भींगा-भींगा होता है। रस में डूबा हुआ, खट्टा और मिर्चदार-रसदार ! पता नहीं, यह उसी रस का असर था या कुछ और, उस दिन अलेक्जेंडर के साथ मैं तुमुल बहस में उलझ पड़ा। मैंने अपनी पत्नी मेरियन की आँखों के निषेध की भी परवाह नहीं की। मेरियन ने ही बताया था कि अलेक्जेंडर का खयाल है कि भारतीय लोग, खासकर बंगाली, बड़े आग-मार्का होते हैं। उसने इतने सारे भारतीय लोगों के साथ काम किया है कि अब वह बँगलादेशी से पश्चिमी बंगालवासी, गुजराती से मराठी तक का फरक फौरन पहचान सकता है। असल में आपका विषय एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए था। यूँ वह बंगालियों को बेहद पसंद करता था। अनुपम दे सरकार नामक कोई सज्जन उसके यहाँ काम करते थे, अब जा चुके हैं। अलेक्जेंडर आज भी उनकी प्रशंसा में पंचमुख रहता है। उनके बारे में उसका कहना है कि कल्पनाशक्ति और बुद्धि का ऐसा मेल आमतौर पर नजर नहीं आता। चूँकि उसे ऐसे ही मिजाज की आदत है, इसलिए यह भी सुनने में आया है कि उसके मन के भीतरी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरियन मेरी बड़ी तरफदारी करती है। अलेक्जेंडर के बंद होते दरवाजे के सामने वह मुस्तैदी से पहरा देती रहती है। इसकी वजह मैंने उससे कभी जानना नहीं चाहा। लेकिन मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर और अपने रिश्ते को लेकर वह खासी मुश्किल में पड़ गई है। रुपहले-घने बाल और कमसिन सूरतवाली वह मोटी-मुटल्ली अधेड़ औरत अलेक्जेंडर रट्लेज की हाईस्कूल की दिलरुबा थी, उसकी स्वीटहार्ट ! हाईस्कूल और ग्रेजुएशन के बाद उसे आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला। इधर अलेक्जेंडर मुट्ठी भर कीमती डिग्रियाँ बटोरकर अब न्यूयॉर्क मेडिकल सेंटर के बायोकैमिस्ट्री का चेयरमैन बन चुका है। यह सच है कि मेरियन की समूची जवानी अपने दूल्हे को ऊँची-ऊँची शिक्षा दिलाने और बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा करने में गुजर गई। अब उन चारों बच्चों के साथ साल के अंतिम दिनों में भी मुलाकात नहीं होती। अकेल्जेंडर अब सत्तावन साल का नौजवान है और मेरियन बेचारी सत्तावन साल की बूढ़ी ! मैंने गौर किया है कि अलेक्जेंडर कम उम्र की छात्राओं के साथ खूब रोमियोगिरी करता है और विवाह-वार्षिकी पर बीवी को हीरे की अँगूठी भी नजर करता है। शातिर खिलाड़ी है, दोनों हाथों से जमकर खेले जा रहा है। मेरियन मुझे अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुना चुकी है हमारी भाषा में एक कहावत प्रचलित है-‘जितनी हँसी, उतने आँसू !’ मेरियन के साथ बिलकुल ऐसा ही हुआ है। अपने स्कूली जीवन में उसने डूब-डूबकर मुहब्बत की, अब सिर्फ बेरंग जीवन गुजार रही है। बहुत संभव है, मैं उसकी नजर में मरदों की विश्वसनीयता का एक प्रतीक बन गया हूँ।
पहले वह मुझसे बाकायदा जिरह करती रहती थी-‘शैरन गिलारी के साथ तुम्हारा कोई चक्कर नहीं है, यह बिल्कुल झूठ है या फिर तुम अपने देश की लड़कियों के अलावा किसी भी लड़की को पसंद नहीं करते। अच्छा, व्हाट एबाउट दैट डॉक्टर्स वाइफ ? डॉक्टर की बीवी के बारे में तुम्हारा क्या खयाल है ?’
मैं उसके सवाल का मजा लेते हुए हँस पड़ता था और यह देखकर उसका चेहरा बुझ जाता था। अगर सभी औरतों के पति का स्वभाव भँवरे जैसा होता तो उसे थोड़ी-बहुत तसल्ली होती। बहरहाल, वह चाहती है कि अलेक्जेंडर के साथ मेरा संपर्क सीमित रहे। हमारी अनौपचारिक बातचीत भी वह निपुण तरीके से मॉनीटर करती रहती है। खैर, उसकी मरजी ! इस बारे में उसकी अपनी वजह होगी लेकिन मैं जान-बूझकर उस निषिद्ध प्रदेश में कदम रख देता हूँ। वह मेरा क्या कर लेगी ? मेरियन की आँखों में खतरे की बत्ती जल उठने के बावजूद मैं अलेक्जेंडर से आराम से उलझता रहता हूँ, जमकर झगड़ा करता हूँ। अलेक्जेंडर भी बिलकुल सगे भाई की तरह बहस करता है। वैसे जब वह ठंडा पड़ भी जाए तो मेरे अंदर की आग बुझ जाएगी, मैं यह वादा भी नहीं करता। बहरहाल, अंत में मेरियन के भंडार से व्हिस्की ऑनरॉक्स निकल ही आती है और सबकुछ धुल-पुँछकर साफ हो जाता है। अब वह चाहे खौलता हुआ लावा हो या हड्सन का बर्फीला जल।
हमारे रास्ते में मेप्ल के पेड़ ज्यादा हैं। चेरी के भी दो-चार पेड़ हैं। मैं देख रहा हूँ, मेप्ल की बड़ी-बड़ी बहारी डालों पर बर्फ की झीनी-सी परत पड़ी हुई है। बेहद खूबसूरत लगती है ये। लेकिन जब आस-पास नजर दौड़ाता हूँ, तो अजीब सी विरक्ति होती है। प्रकृति की ये खूबसूरत बूँदें तभी भली लगती हैं, जब बाहर निकलना हो। जब मैंने यहाँ पहली बार कदम रखा था, न्यूयॉर्क अब उससे भी ज्यादा बेरंग हो आया है। बर्फ की कीचड़ लपेटे रहो तो सर्दी के मारे नाक बहते बच्चे की तरह ही इनसान घिनौना नजर आता है। ऐसे मौसम में कलकत्ता में बचपन-किशोर की रिमझिम की बारिश के दिन याद आने लगते हैं। अतीत का मतलब ही है रूमानियत की परतों में लिपटी यादें ! कलकक्ता की बारिश के जमा पानी में गाय और इनसान के मल-मूत्र क्या बहते-उतराते नहीं रहते ? लेकिन जब भी मैंने परतें उघाड़कर देखा है, अंदर सिर्फ कागज की नाव और रवींद्रनाथ ही नजर आए हैं। ‘दौड़ जाती है आँकी-बाँकी जलधार, खेल-मैदानों के पाट ! कौन नाचता है आज मेघों की जटाएँ उड़ाकर !’ उन सब दिनों की अकाल-शामों के वक्त दफ्तर के लोग घुटनों-घुटनों तक धोती उठाए, एक हाथ में जूते और दूसरे हाथ में एक जोड़ी ईलिश मछली लहराते हुए घर लौटते थे। उनमें मेरे बापी भी हुआ करते थे। पैरों में कीचड़ और चेहरे पर हँसी ! बारिश का दिन होने की वजह से हम सब बिच्छू लड़के बहुत पहले ही घर लौटकर ऊधम मचाए रहते थे। ठनठनिया में कमर-कमर पानी ! बड़े और मँझले भइया तो कॉलेज जा ही नहीं पाते थे। अस्तु, दोपहरी के वक्त खेल शुरु हो जाता था। बड़े और मँझले कैरम बिछाकर बैठ जाते थे।
खेलते-खेलते बड़े भइया ऊँची आवाज में गा उठते थे-‘ए जी, यह कैसा अंतिम दान ?’
‘ना-ना, गया नहीं देकर, मैं विरह-दान !’’ गाने की अंतिम कड़ी, खासी मीड़ देकर मँझले भइया पूरा कर देते थे।
यानी गले-गले जंग जारी रहती थी। इधर, मैं दादी छुटकी और सुमित ट्वेंटी नाइन खेल में जुट जाते थे।
दीदार लहजे में छुटकी की बोली-आवाजों की बारिश जारी रहती थी। मारे गुस्से के जल-भुनकर मैं अपना पार्टनर बदलने को आमादा हो जाता था।
वह छूटते ही मिमियाकर चीख उठती थी-‘प्लीज, बस एक चांस और दे दे, सँझले !’
ऐसे ही पूरी दोपहर ढल जाती थी। दिन बादलों के पीछे जा छिपता था और शाम हो आती थी। अचानक रसोई में ईलिश मछली तलने की खुशबू पाकर मन बौरा जाता था। कैरमबोर्ड जस-का-तस पड़ा रहता था, ताश के पत्ते फर्श चूमने लगते थे, ईलिश की खुशबू हमें नीचे, रसोई की तरफ खींच ले जाती थी। हम सब बड़ी माँ का उठौआ, चूल्हा चारों तरफ से घेर लेते थे। उस झुंड में सुकृत भी शामिल रहता था, यह याद नहीं पड़ता। उन दिनों वह क्या काफी छोटा था ? हम सबके हाथों में माँ की थमाई हुई गरमागरम तले हुए अंडे व मछली की प्लेट मानो ‘प्रोल्यूड’ हुआ करती थी यानी पूर्व तैयारी ! जाहिर था कि रात को खास भोज होने वाला था। मजलिस खूब जमेगी।
आज वह झिर-झिर बर्फ बरसाता दिन बारिश की उन शामों का अमेरिकी संस्करण है। वैसे ईलिश मछली के उपहार का यहाँ कोई अमेरिकी संस्करण नहीं है। यहाँ हठात् छुट्टी का रोमांच भी नहीं है। गाड़ियों पर नजर पड़ते ही मेरा मूड बिगड़ गया है। जाहिर है कुछेक पलों में ही उसी किस्म की किसी गाड़ी के अंदर आपादमस्तक ढका हुआ मैं भी किसी गोरिल्ला जैसा ही नजर आऊँगा। वह दृश्य बिलकुल सुखद नहीं होता।
आज अरात्रिका का जन्मदिन है। हर वर्ष यह दिन एक बार आता ही है, यह पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन इस बार बिलकुल नए रूप में आ रहा है। इस बार उसने तेरह पूरा करके चौदहवें में कदम रखा है। ऐसे अर्थपूर्ण समय में घनघोर आँधी-तूफान का प्राकृतिक आयोजन देखकर मेरा प्राचीन प्राच्य संस्कार कैसा तो घबड़ा उठा है। हक्स्ले रचित किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा था-इनसान हमेशा अपने को दुनिया का केंद्र मानता है, हालाँकि असल में वह कोई नहीं होता। उसे केंद्र करके कुछ भी नहीं होता। उसे केंद्र करके कुछ भी नहीं घटता; लेकिन इनसान है कि बेहद आत्मसजग तरीके से अपने को केंद्रबिंदु समझता रहता है। यह एक किस्म की अहंकार भरी बेवकूफी है, साथी ही तसल्ली भी है। हक्स्ले द्वारा कथित उस किस्म की मानसिकता में, शायद मैं भी फँस गया हूँ। प्रकृति पर ऐसी नाटकीयता मैंने ही आरोपित की है। प्रकृति कोई एब्सर्ड नाटक पेश नहीं करती। प्रकृति का नाटक तो खुद ही अपने में एब्सर्ड होता है। फिर मैं ही ऐसा क्यों सोचता हूँ ? अभी भी बाधा विराजमान है। बाधा और दुविधा। लेकिन मुझे तो किसी-न-किसी फैसले पर पहुँचाना ही है।
ब्रुकलिन का मिजाज क्या इस बार बदल गया ? मुझे तो यह छलनामयी यहूदी ललना नजर आई, जिसने अपने को रहस्य के अवगुंठन में आवृत कर रखा हो। यहाँ ठंड के साथ-साथ हवा भी निहायत बेतरतीब और मस्तमौला है ! सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस ठंड के दौरान ही, कोई-कोई बेहद गुनगुना-सुनहरा दिन भी निकल आता है, फ्रेश फ्रॉम द ओवन-बेक्ड चिंगड़ी मछली की तरह। उस दिन तो अपने बदन से लंबा कोट, दस्ताने मफलर वगैरह उतार फेंकने पड़ते हैं। छुट्टी कहाँ होती है ? मगर छुट्टी का मूड बन जाता है। मेरा मन होता है कि मैं सभी लोगों को आवाज देकर पुकारूँ-‘चलो, आज स्कूल-विस्कूल, ऑफिस दफ्तर नहीं, आज हम सब हाइवे से होकर, बफैलो की तरह दौड़ जाएँ। सड़क के दोनों तरफ, उजले-धुले, ठेठ शहर-दर-शहर; वाटर-पेंटिंग जैसे गंज-कस्बे, गाँव-देहात नजर आएँगे। कुछ-कुछ दूरी पर स्थित मोटलों में कुछेक पल गुजारकर सुबह-सुबह किसी फास्ट फूड ज्वॉएंट में मोटे-मोटे हैंबर्गर और शाम को तीन-चार कोर्स इस्पहानी डिनर खाकर, हम अपनी-अपनी गुफा में लौट आएँगे।’’ लेकिन ये सब खामखयाली बातें यहाँ वीक-एंड के अलावा और किसी वक्त जुबान पर नहीं लाई जा सकतीं। इस महादेश में वह भाषा ही अचल है। लेकिन ऐसे बँधे-बँधाए नियमों के मुताबिक धूमधाम से वीक एंड मनाना मुझे सख्त नापसंद है। अरे, ऐसी जोर-जबरदस्ती की जाए तो आराम भला आराम रह पाता है ?
मैंने गौर किया है कि उत्तर की सर्दी का मौसम मेरे खत्री दोस्त वर्मन की पत्नी के हाथों तैयार किए गए दही-बड़े की तरह भारी-भरकम और भींगा-भींगा होता है। रस में डूबा हुआ, खट्टा और मिर्चदार-रसदार ! पता नहीं, यह उसी रस का असर था या कुछ और, उस दिन अलेक्जेंडर के साथ मैं तुमुल बहस में उलझ पड़ा। मैंने अपनी पत्नी मेरियन की आँखों के निषेध की भी परवाह नहीं की। मेरियन ने ही बताया था कि अलेक्जेंडर का खयाल है कि भारतीय लोग, खासकर बंगाली, बड़े आग-मार्का होते हैं। उसने इतने सारे भारतीय लोगों के साथ काम किया है कि अब वह बँगलादेशी से पश्चिमी बंगालवासी, गुजराती से मराठी तक का फरक फौरन पहचान सकता है। असल में आपका विषय एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए था। यूँ वह बंगालियों को बेहद पसंद करता था। अनुपम दे सरकार नामक कोई सज्जन उसके यहाँ काम करते थे, अब जा चुके हैं। अलेक्जेंडर आज भी उनकी प्रशंसा में पंचमुख रहता है। उनके बारे में उसका कहना है कि कल्पनाशक्ति और बुद्धि का ऐसा मेल आमतौर पर नजर नहीं आता। चूँकि उसे ऐसे ही मिजाज की आदत है, इसलिए यह भी सुनने में आया है कि उसके मन के भीतरी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरियन मेरी बड़ी तरफदारी करती है। अलेक्जेंडर के बंद होते दरवाजे के सामने वह मुस्तैदी से पहरा देती रहती है। इसकी वजह मैंने उससे कभी जानना नहीं चाहा। लेकिन मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर और अपने रिश्ते को लेकर वह खासी मुश्किल में पड़ गई है। रुपहले-घने बाल और कमसिन सूरतवाली वह मोटी-मुटल्ली अधेड़ औरत अलेक्जेंडर रट्लेज की हाईस्कूल की दिलरुबा थी, उसकी स्वीटहार्ट ! हाईस्कूल और ग्रेजुएशन के बाद उसे आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला। इधर अलेक्जेंडर मुट्ठी भर कीमती डिग्रियाँ बटोरकर अब न्यूयॉर्क मेडिकल सेंटर के बायोकैमिस्ट्री का चेयरमैन बन चुका है। यह सच है कि मेरियन की समूची जवानी अपने दूल्हे को ऊँची-ऊँची शिक्षा दिलाने और बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा करने में गुजर गई। अब उन चारों बच्चों के साथ साल के अंतिम दिनों में भी मुलाकात नहीं होती। अकेल्जेंडर अब सत्तावन साल का नौजवान है और मेरियन बेचारी सत्तावन साल की बूढ़ी ! मैंने गौर किया है कि अलेक्जेंडर कम उम्र की छात्राओं के साथ खूब रोमियोगिरी करता है और विवाह-वार्षिकी पर बीवी को हीरे की अँगूठी भी नजर करता है। शातिर खिलाड़ी है, दोनों हाथों से जमकर खेले जा रहा है। मेरियन मुझे अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुना चुकी है हमारी भाषा में एक कहावत प्रचलित है-‘जितनी हँसी, उतने आँसू !’ मेरियन के साथ बिलकुल ऐसा ही हुआ है। अपने स्कूली जीवन में उसने डूब-डूबकर मुहब्बत की, अब सिर्फ बेरंग जीवन गुजार रही है। बहुत संभव है, मैं उसकी नजर में मरदों की विश्वसनीयता का एक प्रतीक बन गया हूँ।
पहले वह मुझसे बाकायदा जिरह करती रहती थी-‘शैरन गिलारी के साथ तुम्हारा कोई चक्कर नहीं है, यह बिल्कुल झूठ है या फिर तुम अपने देश की लड़कियों के अलावा किसी भी लड़की को पसंद नहीं करते। अच्छा, व्हाट एबाउट दैट डॉक्टर्स वाइफ ? डॉक्टर की बीवी के बारे में तुम्हारा क्या खयाल है ?’
मैं उसके सवाल का मजा लेते हुए हँस पड़ता था और यह देखकर उसका चेहरा बुझ जाता था। अगर सभी औरतों के पति का स्वभाव भँवरे जैसा होता तो उसे थोड़ी-बहुत तसल्ली होती। बहरहाल, वह चाहती है कि अलेक्जेंडर के साथ मेरा संपर्क सीमित रहे। हमारी अनौपचारिक बातचीत भी वह निपुण तरीके से मॉनीटर करती रहती है। खैर, उसकी मरजी ! इस बारे में उसकी अपनी वजह होगी लेकिन मैं जान-बूझकर उस निषिद्ध प्रदेश में कदम रख देता हूँ। वह मेरा क्या कर लेगी ? मेरियन की आँखों में खतरे की बत्ती जल उठने के बावजूद मैं अलेक्जेंडर से आराम से उलझता रहता हूँ, जमकर झगड़ा करता हूँ। अलेक्जेंडर भी बिलकुल सगे भाई की तरह बहस करता है। वैसे जब वह ठंडा पड़ भी जाए तो मेरे अंदर की आग बुझ जाएगी, मैं यह वादा भी नहीं करता। बहरहाल, अंत में मेरियन के भंडार से व्हिस्की ऑनरॉक्स निकल ही आती है और सबकुछ धुल-पुँछकर साफ हो जाता है। अब वह चाहे खौलता हुआ लावा हो या हड्सन का बर्फीला जल।
हमारे रास्ते में मेप्ल के पेड़ ज्यादा हैं। चेरी के भी दो-चार पेड़ हैं। मैं देख रहा हूँ, मेप्ल की बड़ी-बड़ी बहारी डालों पर बर्फ की झीनी-सी परत पड़ी हुई है। बेहद खूबसूरत लगती है ये। लेकिन जब आस-पास नजर दौड़ाता हूँ, तो अजीब सी विरक्ति होती है। प्रकृति की ये खूबसूरत बूँदें तभी भली लगती हैं, जब बाहर निकलना हो। जब मैंने यहाँ पहली बार कदम रखा था, न्यूयॉर्क अब उससे भी ज्यादा बेरंग हो आया है। बर्फ की कीचड़ लपेटे रहो तो सर्दी के मारे नाक बहते बच्चे की तरह ही इनसान घिनौना नजर आता है। ऐसे मौसम में कलकत्ता में बचपन-किशोर की रिमझिम की बारिश के दिन याद आने लगते हैं। अतीत का मतलब ही है रूमानियत की परतों में लिपटी यादें ! कलकक्ता की बारिश के जमा पानी में गाय और इनसान के मल-मूत्र क्या बहते-उतराते नहीं रहते ? लेकिन जब भी मैंने परतें उघाड़कर देखा है, अंदर सिर्फ कागज की नाव और रवींद्रनाथ ही नजर आए हैं। ‘दौड़ जाती है आँकी-बाँकी जलधार, खेल-मैदानों के पाट ! कौन नाचता है आज मेघों की जटाएँ उड़ाकर !’ उन सब दिनों की अकाल-शामों के वक्त दफ्तर के लोग घुटनों-घुटनों तक धोती उठाए, एक हाथ में जूते और दूसरे हाथ में एक जोड़ी ईलिश मछली लहराते हुए घर लौटते थे। उनमें मेरे बापी भी हुआ करते थे। पैरों में कीचड़ और चेहरे पर हँसी ! बारिश का दिन होने की वजह से हम सब बिच्छू लड़के बहुत पहले ही घर लौटकर ऊधम मचाए रहते थे। ठनठनिया में कमर-कमर पानी ! बड़े और मँझले भइया तो कॉलेज जा ही नहीं पाते थे। अस्तु, दोपहरी के वक्त खेल शुरु हो जाता था। बड़े और मँझले कैरम बिछाकर बैठ जाते थे।
खेलते-खेलते बड़े भइया ऊँची आवाज में गा उठते थे-‘ए जी, यह कैसा अंतिम दान ?’
‘ना-ना, गया नहीं देकर, मैं विरह-दान !’’ गाने की अंतिम कड़ी, खासी मीड़ देकर मँझले भइया पूरा कर देते थे।
यानी गले-गले जंग जारी रहती थी। इधर, मैं दादी छुटकी और सुमित ट्वेंटी नाइन खेल में जुट जाते थे।
दीदार लहजे में छुटकी की बोली-आवाजों की बारिश जारी रहती थी। मारे गुस्से के जल-भुनकर मैं अपना पार्टनर बदलने को आमादा हो जाता था।
वह छूटते ही मिमियाकर चीख उठती थी-‘प्लीज, बस एक चांस और दे दे, सँझले !’
ऐसे ही पूरी दोपहर ढल जाती थी। दिन बादलों के पीछे जा छिपता था और शाम हो आती थी। अचानक रसोई में ईलिश मछली तलने की खुशबू पाकर मन बौरा जाता था। कैरमबोर्ड जस-का-तस पड़ा रहता था, ताश के पत्ते फर्श चूमने लगते थे, ईलिश की खुशबू हमें नीचे, रसोई की तरफ खींच ले जाती थी। हम सब बड़ी माँ का उठौआ, चूल्हा चारों तरफ से घेर लेते थे। उस झुंड में सुकृत भी शामिल रहता था, यह याद नहीं पड़ता। उन दिनों वह क्या काफी छोटा था ? हम सबके हाथों में माँ की थमाई हुई गरमागरम तले हुए अंडे व मछली की प्लेट मानो ‘प्रोल्यूड’ हुआ करती थी यानी पूर्व तैयारी ! जाहिर था कि रात को खास भोज होने वाला था। मजलिस खूब जमेगी।
आज वह झिर-झिर बर्फ बरसाता दिन बारिश की उन शामों का अमेरिकी संस्करण है। वैसे ईलिश मछली के उपहार का यहाँ कोई अमेरिकी संस्करण नहीं है। यहाँ हठात् छुट्टी का रोमांच भी नहीं है। गाड़ियों पर नजर पड़ते ही मेरा मूड बिगड़ गया है। जाहिर है कुछेक पलों में ही उसी किस्म की किसी गाड़ी के अंदर आपादमस्तक ढका हुआ मैं भी किसी गोरिल्ला जैसा ही नजर आऊँगा। वह दृश्य बिलकुल सुखद नहीं होता।
आज अरात्रिका का जन्मदिन है। हर वर्ष यह दिन एक बार आता ही है, यह पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन इस बार बिलकुल नए रूप में आ रहा है। इस बार उसने तेरह पूरा करके चौदहवें में कदम रखा है। ऐसे अर्थपूर्ण समय में घनघोर आँधी-तूफान का प्राकृतिक आयोजन देखकर मेरा प्राचीन प्राच्य संस्कार कैसा तो घबड़ा उठा है। हक्स्ले रचित किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा था-इनसान हमेशा अपने को दुनिया का केंद्र मानता है, हालाँकि असल में वह कोई नहीं होता। उसे केंद्र करके कुछ भी नहीं होता। उसे केंद्र करके कुछ भी नहीं घटता; लेकिन इनसान है कि बेहद आत्मसजग तरीके से अपने को केंद्रबिंदु समझता रहता है। यह एक किस्म की अहंकार भरी बेवकूफी है, साथी ही तसल्ली भी है। हक्स्ले द्वारा कथित उस किस्म की मानसिकता में, शायद मैं भी फँस गया हूँ। प्रकृति पर ऐसी नाटकीयता मैंने ही आरोपित की है। प्रकृति कोई एब्सर्ड नाटक पेश नहीं करती। प्रकृति का नाटक तो खुद ही अपने में एब्सर्ड होता है। फिर मैं ही ऐसा क्यों सोचता हूँ ? अभी भी बाधा विराजमान है। बाधा और दुविधा। लेकिन मुझे तो किसी-न-किसी फैसले पर पहुँचाना ही है।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book