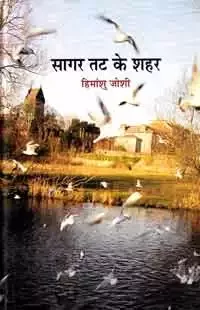|
सामाजिक >> महासागर महासागरहिमांशु जोशी
|
337 पाठक हैं |
||||||
महासागर उन लोगों की दर्द भरी कहानी है जिन्हें नियति ने अलग-2 स्वनिर्मित द्विपों में निर्वासित होने के लिए विवश किया है
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘महासागर’
उन लोगों की दर्द भरी कहानी है,
जिन्हें नियती ने अलग-अलग स्वनिर्मित द्वीपों में
निर्वासित होने के लिए विवश किया है।
इसमें जिस नए संसार की संरचना की गई है-
अनेक संसारों को जोड़कर-उसका
अलग-अलग रुप ही नहीं, रंग ही नहीं,
अपनी अलग एक पहचान भी है।
साकेत के माध्यम से अनेक आदर्शोन्मुख
साकेतों के प्रतिबिम्ब मिलेंगे।
दीप’दी के माध्यम से अनेक संघर्षरत
दीप’दी दिखलाई देंगी।
इसमें निहित ‘पर के लिए स्वयं का
विसर्जन भाव’ बहुत कुछ सोचने के लिए
विवश करता है।
सरल, सहज, स्वाभाविक घटनाओं के ताने-बाने
से बुनी इसकी कहानी मात्र
मानव-संबंधों की कहानी ही नहीं, बल्कि
वर्तमान की जीती-जागती तस्वीर भी है।
निर्वासित द्वीपों की निर्जन पृष्ठभूमि पर
लिखी प्रस्तुत कृति अपने समय का एक
प्रामाणिक दस्तावेज है-
एक चिरंतन चिर सत्य व्यथा-कथा भी।
उन लोगों की दर्द भरी कहानी है,
जिन्हें नियती ने अलग-अलग स्वनिर्मित द्वीपों में
निर्वासित होने के लिए विवश किया है।
इसमें जिस नए संसार की संरचना की गई है-
अनेक संसारों को जोड़कर-उसका
अलग-अलग रुप ही नहीं, रंग ही नहीं,
अपनी अलग एक पहचान भी है।
साकेत के माध्यम से अनेक आदर्शोन्मुख
साकेतों के प्रतिबिम्ब मिलेंगे।
दीप’दी के माध्यम से अनेक संघर्षरत
दीप’दी दिखलाई देंगी।
इसमें निहित ‘पर के लिए स्वयं का
विसर्जन भाव’ बहुत कुछ सोचने के लिए
विवश करता है।
सरल, सहज, स्वाभाविक घटनाओं के ताने-बाने
से बुनी इसकी कहानी मात्र
मानव-संबंधों की कहानी ही नहीं, बल्कि
वर्तमान की जीती-जागती तस्वीर भी है।
निर्वासित द्वीपों की निर्जन पृष्ठभूमि पर
लिखी प्रस्तुत कृति अपने समय का एक
प्रामाणिक दस्तावेज है-
एक चिरंतन चिर सत्य व्यथा-कथा भी।
दो शब्द
कुछ घटनाओं को निकट से देखा, कुछ व्यक्तियों को निकट से परखा साकेत, दीप,
छाया, नीना—सभी पात्र किसी-न-किसी रूप में मेरे चारों ओर बिखरे रहे।
उन सबको सहेजकर, यहाँ एकत्रित करने का प्रयास भर मैंने किया है।
जो रचना जीवन के जितना निकट रहती है, वह उतनी ही स्वाभाविक होती है—शुरू से ही मेरी यह मान्यता रही है। इसलिए जहाँ तक बन सका, ‘करिश्मा’ दिखाने से मैं सदैव बचता रहा हूँ।
दादा बाबू को ठेला चलाते हुए मैंने ही नहीं, बहुतों ने देखा है। मुझे वह दिन अब तक याद है, जब नगर निगम की गाड़ी उसका ठेला उठाकर ले गई थी, और दिन-भर वह पागलों की तरह घर-घर फिरता रहा था। दीप जिस विद्यालय में पढ़ाती थी, वह मेरे घर से अधिक दूर नहीं था। साकेत वर्षों तक मेरा अभिन्न मित्र रहा। युक्लिप्टस का वह पेड़ अब भी ज्यों-का-त्यों उसी तरह खड़ा है। हां, कुछ बूढ़ा अवश्य हो गया है। जिस मकान में साकेत रहता था, उसमें अब कोई और रहता है उधर से होकर कभी गुजरता हूँ तो चलचित्र के दृश्यों की तरह बहुत-कुछ आँखों के आगे घूमने लगता है। यह सब लिखते समय न जाने क्यों यह लगता है कि इन सबके साथ-साथ कहीं मैं स्वयं भी तो एक पात्र नहीं ! जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे कहीं मैं अपने ही विषय में तो नहीं लिख रहा ! हो सकता है, पढ़ते समय कहीं आपको भी अपना प्रतिबिंब दीखे ! अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना प्रयत्न सफल समझूँगा।
जो रचना जीवन के जितना निकट रहती है, वह उतनी ही स्वाभाविक होती है—शुरू से ही मेरी यह मान्यता रही है। इसलिए जहाँ तक बन सका, ‘करिश्मा’ दिखाने से मैं सदैव बचता रहा हूँ।
दादा बाबू को ठेला चलाते हुए मैंने ही नहीं, बहुतों ने देखा है। मुझे वह दिन अब तक याद है, जब नगर निगम की गाड़ी उसका ठेला उठाकर ले गई थी, और दिन-भर वह पागलों की तरह घर-घर फिरता रहा था। दीप जिस विद्यालय में पढ़ाती थी, वह मेरे घर से अधिक दूर नहीं था। साकेत वर्षों तक मेरा अभिन्न मित्र रहा। युक्लिप्टस का वह पेड़ अब भी ज्यों-का-त्यों उसी तरह खड़ा है। हां, कुछ बूढ़ा अवश्य हो गया है। जिस मकान में साकेत रहता था, उसमें अब कोई और रहता है उधर से होकर कभी गुजरता हूँ तो चलचित्र के दृश्यों की तरह बहुत-कुछ आँखों के आगे घूमने लगता है। यह सब लिखते समय न जाने क्यों यह लगता है कि इन सबके साथ-साथ कहीं मैं स्वयं भी तो एक पात्र नहीं ! जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे कहीं मैं अपने ही विषय में तो नहीं लिख रहा ! हो सकता है, पढ़ते समय कहीं आपको भी अपना प्रतिबिंब दीखे ! अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना प्रयत्न सफल समझूँगा।
हिमांशु जोशी
महासागर
वह असमंजस से कुछ सोच ही रहा था कि हौले से दरवाज़ा खुला। रूप आई और चाय
का प्याला रखकर चली गई। साकेत ने एक बार रूप की ओर देखा, फिर प्याले की ओर।
रूप के लिए एक धोती चाहिए। पिछले दिनों से वह एक ही धोती से किसी तरह गुज़ारा कर रही है। अन्नी पिकनिक के लिए पैसे माँगता था। कहता था-उसकी क्लास के सभी विद्यार्थी जा रहे हैं, वह बिना जूता कैसे जाएगा ? छाया घर से बाहर कम निकलती है। उसकी आँखें बचपन से ही खराब हैं। पर अब उसे उतना भी नहीं दीखता। घर की चारदीवारी के भीतर बैठी रूप के कपड़ों से तन ढांप लेती है।
वह सोचता, परीक्षाएँ समाप्त हो जातीं तो वह एक-दो ट्यूसनें और ढूंढ़ लेता। फिर पार्टटाइम काम की तलाश करता। किंतु परीक्षाएं अभी भी आरंभ नहीं हुईं। फिर कब समाप्त होंगी ? कब ? वह कुछ उलझ-सा गया।
प्याला अपनी ओर बढ़ाया। उसके ऊपर भाप की पतली-सी, पारदर्शी, दुहरी लकीर की ओर वह ताकता रहा...
सिप्-सिप्...एक दो बार होंठों से छुआ कर प्याला उसने नीचे रख दिया। जहाँ पहले रखा था—वहाँ पर प्याले के पेंदे का एक गोल निशान-सा रह गया था—गीला...
वह अंगड़ाई लेता हुआ कुछ सोचकर उठा। खिड़की उसने आधी खोल दी। धूप का एक तिरछा टुकड़ा, अधखुली शीशे की दीवार चीरकर फर्श पर फैला, एक आकृति बना रहा था। कमरे में बिखरी धूल उजली हो आई थी, जैसे सारी वस्तुओं के ऊपर का आवरण हट गया और सब नग्न हो आई हों, अपने वास्तविक रूप में।
कुर्सी थोड़ी-सी उसने आगे सरकाई, ताकि धूप का पूरा पीला चकत्ता उसे घेर ले। वह अब कुर्सी पर, पीठ के बल आराम से बैठ गया। पाँवों को दूर तक फैलाया-तानकर और फिर छत की ओर निगाहें टिकाए, मानो कुछ खोजने लगा हो।
सामने दीवार पर टँगे एक धुँधले-से चित्र पर उसकी निगाहें अनायास अटक आईं।
खादी के कपड़े। बढ़ी हुई दाढ़ी। बँधे हुए हाथ। पाँवों पर भारी-भारी बेड़ियाँ। चौखट के ऊपर मुरझाए फूलों की माला, जो धूल और धुएँ के कारण कुछ-कुछ धुमरैली हो आई है।
यह चित्र उसके दिवंगत पिता का है। पता नहीं, इसे कौन, कैसे, कब खींचकर यहाँ लाया था ! माँ जब तक जिंदा थीं, उनके पूजा के देवताओं के पास यह भी रखा रहता था। हर पंद्रह अगस्त के दिन माँ इस पर ताज़ा फूलों का माला चढ़ाती थीं। पिताजी का श्राद्ध माँ वर्ष के इसी दिन मनातीं। यह माला, जो अब तक टंगी है, माँ के जीवन के अंतिम पंद्रह अगस्त की थी...शायद वह...शायद
‘‘भैया, आज छुट्टी है ?’’
रूप ने जगाया तो साकेत अचकचाया हुआ जागा। गोद में गिरी, अधखुली मोटी किताब उसने बंद करके मेज़ पर रखा दी। प्याले में बची सारी ठंडी चाय एक ही घूँट में गटक गया।
यों ही झट-पट हाथ-मुँह धोकर कपड़े बदलने लगा। अपना हमेशा का बंद गले का खादी का ऊनी कोट उसने तन पर डाला। चप्पलें पहनीं। बिना शीशे में देखे बाल बनाए और दो-तीन पुस्तकें बगल में दबाए, सीटी बजाता हुआ सीढ़ियाँ पार कर रहा था कि उसे भीतर रोने-झगड़ने की जैसी आवाज़ सुनाई दी।
अंतिम सीढ़ी पर पाँव गिरता-गिरता रुक गया।
‘‘रूप !’’
रात के मैले बर्तन माँज रही थी रूप। आवाज़ सुनकर वैसी ही हड़बड़ाती हुई आई। काले-काले हाथों को शरीर से दूर उठाए वह झिझकती-सी प्रतिच्छाया की तरह खड़ी हो गई।
‘‘भीतर कौन रो रहा है ?’’
‘‘अन्नी होगा, भैया !’’
‘‘क्यों, क्या हुआ ?’’
‘‘कुछ नहीं।’’ उसने केवल सिर हिलाया।
‘‘तुमने मारा होगा ?’’ उसने प्यार से डपटकर कहा।
रूप कुछ उत्तर दे, उससे पहले दीवार के सहारे खड़ी छाया बोल पड़ी—अम्मी ने मारा, दद्दा !’’
‘‘क्यों ?’’
‘‘रोटी माँगता था।’’
‘‘तो दे दो ! इसमें रोने की क्या बात है ?’’
किसी ने उसकी बात का कोई उत्तर न दिया। सब चुपचाप उसकी आकृति की ओर देखते रहे तो वह कुछ सहम-सा आया।
उसका हाथ ठोढ़ी पर टिका। माथे पर किंचित बल पड़ा। होठों को जीभ की नोक से भिगोता हुआ बोला, ‘‘राशन खत्म हो गया क्या—?’’
रूप इस बार भी चुप रही...बोली नहीं।
साकेत के पाँव जहाँ पर थे, वहीं पर इस्पात की तरह जम गए। रात का भोजन वह स्वयं इधर-उधर कहीं कर लेता है। कल रात जब वह देर से लौटा तो सब सो चुके थे। चूल्हा बुझ गया था। कल रात भी ऐसा शोरगुल था। कल रात भी छोटी माँ बड़ी बेरहमी से बच्चों को मार रही थीं।
दाँतों की दोहरी पाटी के बीच दबे उसके निचले होंठ पर इतना दबाव पड़ा कि मांस पर दो-तीन गहरे काले निशान-से छूट गए।
‘‘तुमने कल बतलाया क्यों नहीं ?’’
साकेत ने इस तरह पूछा कि रूप सहम गई।
‘‘मैंने कहा था न कि जब कोई चीज़ खत्म होने लगे तो उससे एक-दो दिन पहेल बतला दिया करो !’’
‘‘बतलाया तो था !’’ डरते-डरते रूप ने कहा, ‘‘आप पढ़ रहे थे। शायद सुना न हो !’’
‘‘हाँ, बतलाया था !’’ साकेत ने जैसे अपने से पूछा।
इधर पता नहीं क्या हो गया है, हर बात वह भूल जाता है...कल शाम पैन ढूंढ़ने में सारा कमरा छान मारा, पर पैन जेब में टँगा था। मामा जी का परसों खत आया था कि लिफाफे पर टिकट लगाना रह गया था...प्रबोध लिखता है—साठ पैसे के स्टैम्प्स एक ही एनवलप पर लगाने का अर्थ ?
पेड़ों की छाया फर्श पर लुढ़के पानी की तरह बिखरी है। खाली सड़क बहुत चौड़ी लग रही है। कॉरपोरेशन के पार्क पर कहीं-कहीं कुछ पीले फूल चमक रहे हैं। धूप में पत्तियों का गहरा हरा रंग...
साकेत इतना चलने पर भी जैसे वहीं खड़ा हो, जहाँ से चला था। उसे कुछ सूझ नहीं रही था कि किधर चले !
रतन बीसलपुर से अब तक लौटा न होगा...ताई—रतन की माँ अभी तक अस्पताल में होंगी। घर पर ताला होगा...
सामने खड़े ताड़ के वृक्ष की ऊँचाई आज सचमुच बहुत बढ़ आई है !
राशन वाले की दुकान की ओर जाने की हिम्मत नहीं हो पाती। उसका पिछला बकाया अब तक चुकाया न जा सका है। आगे कब चुकाया जा सकेगा, भरोसा नहीं !
आज रविवार है। छुट्टी है। उसे पूरा यकीन है दीप’दी घर में ही होगी। हाँ, सचमुच दीप’दी घर में ही है। खादी के बड़े-बड़े फूलों वाले मोटे परदे, अधखुली आसमानी खिड़की, आबनूसी कपाट, दीवार छत, फर्श, चारों ओर दरवाजे-ही-दरवाजे !
बाहर एक स्कूटर खड़ा है।
दीप’दी कहती थी—शिशिर बाबू उसके ट्रांसफर पर तुले हैं। शिशिर बाबू पशु हैं। शिशिर बाबू ‘मांसाहारी’ पशु हैं। शिशिर बाबू खादी के कपड़े पहनते हैं और मनुष्य का मांस खाते हैं...।
साकेत के पाँव बढ़ नहीं पाते। हर कदम बड़ी मुश्किल से उठकर, वहीं पर जम जाता है। आधी सीढ़ियों पर ही कुछ क्षण रहकर वह खट्-खट् करता लौट पड़ता है।
जाड़े के दिन हैं—सात बजने में समय ही कितना लगता है ?
अभी आधे घंटे की ही तो देरी हुई है—वह सोचता है। अच्छा है तब तक ट्यूशन ही पढ़ा आए ! कल से उसके छमाही इम्तिहान हैं।
बिना अधिक सोचे उसके पाँव किसी सँकरी गली की ओर मुड़ पड़ते हैं, जहाँ नीम के पेड़ पर बहुत-से कौवे बैठे रहते हैं, जहाँ सड़क के दोनों ओर मकानों की बहुत-सी खिड़कियाँ खुली रहती हैं, जहाँ हर खिड़की की चौखट से एक औरत झाँकती दिखलाई देती है।
भले लोग इस गली से होकर नहीं गुजरते, पर साकेत का रास्ता इसी बदनाम गली से होकर जाता है। पर कहीं वह देखता नहीं—खजुराहों के ये सदियों पुराने सजीव चित्र उसे अर्थहीन लगते हैं।
वह दूसरी गली के किसी बड़े मकान में ओझल हो जाता है।
रूप के लिए एक धोती चाहिए। पिछले दिनों से वह एक ही धोती से किसी तरह गुज़ारा कर रही है। अन्नी पिकनिक के लिए पैसे माँगता था। कहता था-उसकी क्लास के सभी विद्यार्थी जा रहे हैं, वह बिना जूता कैसे जाएगा ? छाया घर से बाहर कम निकलती है। उसकी आँखें बचपन से ही खराब हैं। पर अब उसे उतना भी नहीं दीखता। घर की चारदीवारी के भीतर बैठी रूप के कपड़ों से तन ढांप लेती है।
वह सोचता, परीक्षाएँ समाप्त हो जातीं तो वह एक-दो ट्यूसनें और ढूंढ़ लेता। फिर पार्टटाइम काम की तलाश करता। किंतु परीक्षाएं अभी भी आरंभ नहीं हुईं। फिर कब समाप्त होंगी ? कब ? वह कुछ उलझ-सा गया।
प्याला अपनी ओर बढ़ाया। उसके ऊपर भाप की पतली-सी, पारदर्शी, दुहरी लकीर की ओर वह ताकता रहा...
सिप्-सिप्...एक दो बार होंठों से छुआ कर प्याला उसने नीचे रख दिया। जहाँ पहले रखा था—वहाँ पर प्याले के पेंदे का एक गोल निशान-सा रह गया था—गीला...
वह अंगड़ाई लेता हुआ कुछ सोचकर उठा। खिड़की उसने आधी खोल दी। धूप का एक तिरछा टुकड़ा, अधखुली शीशे की दीवार चीरकर फर्श पर फैला, एक आकृति बना रहा था। कमरे में बिखरी धूल उजली हो आई थी, जैसे सारी वस्तुओं के ऊपर का आवरण हट गया और सब नग्न हो आई हों, अपने वास्तविक रूप में।
कुर्सी थोड़ी-सी उसने आगे सरकाई, ताकि धूप का पूरा पीला चकत्ता उसे घेर ले। वह अब कुर्सी पर, पीठ के बल आराम से बैठ गया। पाँवों को दूर तक फैलाया-तानकर और फिर छत की ओर निगाहें टिकाए, मानो कुछ खोजने लगा हो।
सामने दीवार पर टँगे एक धुँधले-से चित्र पर उसकी निगाहें अनायास अटक आईं।
खादी के कपड़े। बढ़ी हुई दाढ़ी। बँधे हुए हाथ। पाँवों पर भारी-भारी बेड़ियाँ। चौखट के ऊपर मुरझाए फूलों की माला, जो धूल और धुएँ के कारण कुछ-कुछ धुमरैली हो आई है।
यह चित्र उसके दिवंगत पिता का है। पता नहीं, इसे कौन, कैसे, कब खींचकर यहाँ लाया था ! माँ जब तक जिंदा थीं, उनके पूजा के देवताओं के पास यह भी रखा रहता था। हर पंद्रह अगस्त के दिन माँ इस पर ताज़ा फूलों का माला चढ़ाती थीं। पिताजी का श्राद्ध माँ वर्ष के इसी दिन मनातीं। यह माला, जो अब तक टंगी है, माँ के जीवन के अंतिम पंद्रह अगस्त की थी...शायद वह...शायद
‘‘भैया, आज छुट्टी है ?’’
रूप ने जगाया तो साकेत अचकचाया हुआ जागा। गोद में गिरी, अधखुली मोटी किताब उसने बंद करके मेज़ पर रखा दी। प्याले में बची सारी ठंडी चाय एक ही घूँट में गटक गया।
यों ही झट-पट हाथ-मुँह धोकर कपड़े बदलने लगा। अपना हमेशा का बंद गले का खादी का ऊनी कोट उसने तन पर डाला। चप्पलें पहनीं। बिना शीशे में देखे बाल बनाए और दो-तीन पुस्तकें बगल में दबाए, सीटी बजाता हुआ सीढ़ियाँ पार कर रहा था कि उसे भीतर रोने-झगड़ने की जैसी आवाज़ सुनाई दी।
अंतिम सीढ़ी पर पाँव गिरता-गिरता रुक गया।
‘‘रूप !’’
रात के मैले बर्तन माँज रही थी रूप। आवाज़ सुनकर वैसी ही हड़बड़ाती हुई आई। काले-काले हाथों को शरीर से दूर उठाए वह झिझकती-सी प्रतिच्छाया की तरह खड़ी हो गई।
‘‘भीतर कौन रो रहा है ?’’
‘‘अन्नी होगा, भैया !’’
‘‘क्यों, क्या हुआ ?’’
‘‘कुछ नहीं।’’ उसने केवल सिर हिलाया।
‘‘तुमने मारा होगा ?’’ उसने प्यार से डपटकर कहा।
रूप कुछ उत्तर दे, उससे पहले दीवार के सहारे खड़ी छाया बोल पड़ी—अम्मी ने मारा, दद्दा !’’
‘‘क्यों ?’’
‘‘रोटी माँगता था।’’
‘‘तो दे दो ! इसमें रोने की क्या बात है ?’’
किसी ने उसकी बात का कोई उत्तर न दिया। सब चुपचाप उसकी आकृति की ओर देखते रहे तो वह कुछ सहम-सा आया।
उसका हाथ ठोढ़ी पर टिका। माथे पर किंचित बल पड़ा। होठों को जीभ की नोक से भिगोता हुआ बोला, ‘‘राशन खत्म हो गया क्या—?’’
रूप इस बार भी चुप रही...बोली नहीं।
साकेत के पाँव जहाँ पर थे, वहीं पर इस्पात की तरह जम गए। रात का भोजन वह स्वयं इधर-उधर कहीं कर लेता है। कल रात जब वह देर से लौटा तो सब सो चुके थे। चूल्हा बुझ गया था। कल रात भी ऐसा शोरगुल था। कल रात भी छोटी माँ बड़ी बेरहमी से बच्चों को मार रही थीं।
दाँतों की दोहरी पाटी के बीच दबे उसके निचले होंठ पर इतना दबाव पड़ा कि मांस पर दो-तीन गहरे काले निशान-से छूट गए।
‘‘तुमने कल बतलाया क्यों नहीं ?’’
साकेत ने इस तरह पूछा कि रूप सहम गई।
‘‘मैंने कहा था न कि जब कोई चीज़ खत्म होने लगे तो उससे एक-दो दिन पहेल बतला दिया करो !’’
‘‘बतलाया तो था !’’ डरते-डरते रूप ने कहा, ‘‘आप पढ़ रहे थे। शायद सुना न हो !’’
‘‘हाँ, बतलाया था !’’ साकेत ने जैसे अपने से पूछा।
इधर पता नहीं क्या हो गया है, हर बात वह भूल जाता है...कल शाम पैन ढूंढ़ने में सारा कमरा छान मारा, पर पैन जेब में टँगा था। मामा जी का परसों खत आया था कि लिफाफे पर टिकट लगाना रह गया था...प्रबोध लिखता है—साठ पैसे के स्टैम्प्स एक ही एनवलप पर लगाने का अर्थ ?
पेड़ों की छाया फर्श पर लुढ़के पानी की तरह बिखरी है। खाली सड़क बहुत चौड़ी लग रही है। कॉरपोरेशन के पार्क पर कहीं-कहीं कुछ पीले फूल चमक रहे हैं। धूप में पत्तियों का गहरा हरा रंग...
साकेत इतना चलने पर भी जैसे वहीं खड़ा हो, जहाँ से चला था। उसे कुछ सूझ नहीं रही था कि किधर चले !
रतन बीसलपुर से अब तक लौटा न होगा...ताई—रतन की माँ अभी तक अस्पताल में होंगी। घर पर ताला होगा...
सामने खड़े ताड़ के वृक्ष की ऊँचाई आज सचमुच बहुत बढ़ आई है !
राशन वाले की दुकान की ओर जाने की हिम्मत नहीं हो पाती। उसका पिछला बकाया अब तक चुकाया न जा सका है। आगे कब चुकाया जा सकेगा, भरोसा नहीं !
आज रविवार है। छुट्टी है। उसे पूरा यकीन है दीप’दी घर में ही होगी। हाँ, सचमुच दीप’दी घर में ही है। खादी के बड़े-बड़े फूलों वाले मोटे परदे, अधखुली आसमानी खिड़की, आबनूसी कपाट, दीवार छत, फर्श, चारों ओर दरवाजे-ही-दरवाजे !
बाहर एक स्कूटर खड़ा है।
दीप’दी कहती थी—शिशिर बाबू उसके ट्रांसफर पर तुले हैं। शिशिर बाबू पशु हैं। शिशिर बाबू ‘मांसाहारी’ पशु हैं। शिशिर बाबू खादी के कपड़े पहनते हैं और मनुष्य का मांस खाते हैं...।
साकेत के पाँव बढ़ नहीं पाते। हर कदम बड़ी मुश्किल से उठकर, वहीं पर जम जाता है। आधी सीढ़ियों पर ही कुछ क्षण रहकर वह खट्-खट् करता लौट पड़ता है।
जाड़े के दिन हैं—सात बजने में समय ही कितना लगता है ?
अभी आधे घंटे की ही तो देरी हुई है—वह सोचता है। अच्छा है तब तक ट्यूशन ही पढ़ा आए ! कल से उसके छमाही इम्तिहान हैं।
बिना अधिक सोचे उसके पाँव किसी सँकरी गली की ओर मुड़ पड़ते हैं, जहाँ नीम के पेड़ पर बहुत-से कौवे बैठे रहते हैं, जहाँ सड़क के दोनों ओर मकानों की बहुत-सी खिड़कियाँ खुली रहती हैं, जहाँ हर खिड़की की चौखट से एक औरत झाँकती दिखलाई देती है।
भले लोग इस गली से होकर नहीं गुजरते, पर साकेत का रास्ता इसी बदनाम गली से होकर जाता है। पर कहीं वह देखता नहीं—खजुराहों के ये सदियों पुराने सजीव चित्र उसे अर्थहीन लगते हैं।
वह दूसरी गली के किसी बड़े मकान में ओझल हो जाता है।
दो
‘‘सर, आज आपको फिर देर हो गई है, सर-
!’’
साकेत को ऐसे सम्बोधन अच्छे नहीं लगते। प्रत्युत्तर में वह कुछ नहीं कहता। रोज़ की तरह हौले से कुर्सी खींचकर धँस पड़ता है।
लड़की की निगाहें पहले से खुली पुस्तक पर अब जमी हैं।
‘‘क्या पढ़ा जा रहा है ?’’
साकेत को ऐसे सम्बोधन अच्छे नहीं लगते। प्रत्युत्तर में वह कुछ नहीं कहता। रोज़ की तरह हौले से कुर्सी खींचकर धँस पड़ता है।
लड़की की निगाहें पहले से खुली पुस्तक पर अब जमी हैं।
‘‘क्या पढ़ा जा रहा है ?’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book