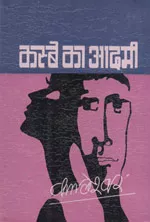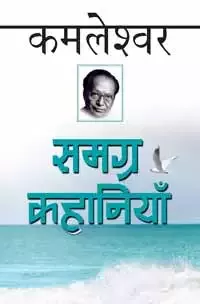|
कहानी संग्रह >> कस्बे का आदमी कस्बे का आदमीकमलेश्वर
|
213 पाठक हैं |
||||||
यह पुस्तक समान्तर कहानी आन्दोलन के प्रथम पुरुष कमलेश्वर का महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
हिन्दी के सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार, नई कहानी आन्दोलन के प्रमुख
प्रवक्ता तथा समान्तर कहानी आन्दोलन के प्रथम पुरुष कमलेश्वर का
महत्त्पूर्ण कहानी-संग्रह।
यह कहानी-संग्रह कमलेश्वर की कथा-यात्रा की महत्त्वपूर्ण कड़ी है। ‘राजा निरबंसिया’ के बाद ‘कस्बे का आदमी’ कमलेश्वर का दूसरा कहानी-संग्रह था जिसने हिन्दी कहानी के क्षेत्र में हलचल मचा दी थी।
काफ़ी समय से अप्राप्य ‘कस्बे के आदमी’ का नाम संस्करण...
यह कहानी-संग्रह कमलेश्वर की कथा-यात्रा की महत्त्वपूर्ण कड़ी है। ‘राजा निरबंसिया’ के बाद ‘कस्बे का आदमी’ कमलेश्वर का दूसरा कहानी-संग्रह था जिसने हिन्दी कहानी के क्षेत्र में हलचल मचा दी थी।
काफ़ी समय से अप्राप्य ‘कस्बे के आदमी’ का नाम संस्करण...
भूमिका
‘‘राजा निरबंसिया’ के बाद यह मेरा दूसरा
कहानी संग्रह
है। इसमें अपेक्षाकृत छोटी कहानियाँ ही हैं। आज की कहानी का रूप बहुत बदल
गया है, अब वह केवल एक बात ही नहीं कहती, जीवन के एक खण्ड, और उस खण्ड को
समग्रता में प्रस्तुत करने की चेष्टा करती है। वह सामान्य की समर्थक है और
साथ ही विशिष्ट की पोषक। इसीलिए कभी-कभी सामान्य कहानियाँ विशिष्ट को
प्रेषित करती जान पड़ती हैं और विशिष्ट कहानियाँ सामान्य को। सामान्य को
विशिष्ट बना देने का गुण मुख्यतः शैली-शिल्प के अधीन है और विशिष्टता को
सामान्यता में परिणत करने का कौशल लेखक की कला का सामाजिक धर्म।
इसी प्रक्रिया से आज रोचकता की रक्षा भी हो रही है। ऐसे नए प्रयासों में आज का कहानीकार सतर्कता से संलग्न है, पर ये प्रयास पिछले को नकारने का दम्भ नहीं करते, उसी सम्पदा और परम्परा से विकसित हो रहे हैं। कहानी की उसी अविरल और अबाध धारा ने प्रसार पाया है, और वह नये जीवन-स्थलों, सत्यों और संवेदनाओं तक पहुँची है।
अपनी इन कहानियों के संबंध में मैं क्या कहूँ ? इनमें से दो-तीन कहानियाँ पहले की लिखी हुई हैं, जो कारणवश ‘राजा निरबंसिया’ संग्रह में नहीं जा सकी थीं। इस संग्रह की कई कहानियों में क़स्बे के जीवन–चित्र हैं। किसी क्षेत्र के प्रति इतना लगाव ‘व्यापकता’ में बाधा माना जा सकता है, पर मैं यह स्वीकार नहीं कर पाता। लेखक का मानस भी एक ही होता है, उसी से सारी रचनाएँ निःसृत होती हैं, यदि वे विविध और व्यापक हो सकती हैं तो क्षेत्र-विशेष उसमें सहायक ही होगा, बाधक नहीं। वह जीवन मानस है, और उसमें उठने वाले ज्वार, संकल्प-विकल्प, संघर्ष और संवेदनाएँ कभी नहीं चूक सकतीं।
इसी प्रक्रिया से आज रोचकता की रक्षा भी हो रही है। ऐसे नए प्रयासों में आज का कहानीकार सतर्कता से संलग्न है, पर ये प्रयास पिछले को नकारने का दम्भ नहीं करते, उसी सम्पदा और परम्परा से विकसित हो रहे हैं। कहानी की उसी अविरल और अबाध धारा ने प्रसार पाया है, और वह नये जीवन-स्थलों, सत्यों और संवेदनाओं तक पहुँची है।
अपनी इन कहानियों के संबंध में मैं क्या कहूँ ? इनमें से दो-तीन कहानियाँ पहले की लिखी हुई हैं, जो कारणवश ‘राजा निरबंसिया’ संग्रह में नहीं जा सकी थीं। इस संग्रह की कई कहानियों में क़स्बे के जीवन–चित्र हैं। किसी क्षेत्र के प्रति इतना लगाव ‘व्यापकता’ में बाधा माना जा सकता है, पर मैं यह स्वीकार नहीं कर पाता। लेखक का मानस भी एक ही होता है, उसी से सारी रचनाएँ निःसृत होती हैं, यदि वे विविध और व्यापक हो सकती हैं तो क्षेत्र-विशेष उसमें सहायक ही होगा, बाधक नहीं। वह जीवन मानस है, और उसमें उठने वाले ज्वार, संकल्प-विकल्प, संघर्ष और संवेदनाएँ कभी नहीं चूक सकतीं।
तीन दिन पहले की रात
मेरे घर आने-जाने वालों की कमी नहीं थी। शाम का वक़्त इसी में चला जाता।
दिवाकर आता था, पर उसका आना धीरे-धीरे कम हो गया। उन दिनों जितेन बहुत आता
था और फिर उसके बाद अमर। वे सब बातें मुझे याद आती हैं। यदि मैं अपने
पिछले क्षणों में वापस लौट सकती तो कितना अच्छा होता !
आज सोचती हूँ तो मन भर-भर आता है। कितने बड़े झूठ और प्रवंचना में हम साँस ले रहे हैं। सुरक्षा, काहे की ? जीवन की ! और यह पैसा और पद ? क्या यही जीवन की सम्पूर्ण प्राप्ति है ? मुझे घृणा होती है। क्या यही जीने का मतलब है और क्या यही आवश्यक है कि एक पुरुष अपनी प्रतिष्ठा की बाँहों में घेरकर भौतिक सुविधाओं से भर दे, जीवन की यह झूठी सुरक्षा दे दे ? प्यार करे ? शारीरिक सम्बन्ध रखे, क्लब और होटलों में ले जाये, पार्टियों में पत्नी को अप्सरा बनाकर औरों की ईर्ष्या में सुख पाये ?
यही हमारा जीवन है, स्वतंत्रता और सभ्यता का जीवन। यह नारी स्वतंत्रता हाथी के दाँत हैं, जिन्हें हर घराना खूबसूरती के लिए लगाए हुए है ! सारी लड़कियाँ स्वतंत्र हैं, वे प्यार कर सकती हैं, घृणा कर सकती हैं, लेकिन जो चाहती हैं वह नहीं कर सकतीं। वे शादी से पहले एकान्त स्थानों में घूम सकती हैं, प्रेम का हर नाटक कर सकती हैं, यह आज़ादी नहीं तो क्या ? मैं भी घूमी हूँ। युवकों के संसर्ग में आयी हूँ। प्यार छिपा-छिपाकर नहीं, दिखा-दिखाकर किया है और इस बात पर विश्वास करती थी कि अन्तिम और गहनतम प्रेम वही होता है, जो अन्त में हो।
लेकिन वे दिन आज याद आते हैं। उन्हें कैसे भूल जाऊँ ? शाम को आने वाले हर परिचित और रिश्तेदार का स्वागत मैं मुसकराकर करती थी। हमारे घरों की शामें इसीलिए होती हैं। सच, तब मुझे यह अच्छा लगता था। विशेषकर इसलिए कि दिवाकर आता था। शाम होते ही डैडी क्लीनिक के लिए तैयार होने लगते। ममी ऐसे तैयार होती, जैसे यह सब करना स्वास्थ्य और ताज़गी के लिए आवश्यक हो। मेरी नसों में बिजली दौड़ जाती। शाम ही तो सचमुच मेरे लिए होती थी। मैं साड़ी बदलती, उसका रंग चुनती, मौसम देखकर रिबनों के रंग बदलती। आँखों में लंबी सलाई से काजल डालती, फिर ढेर-सा सेण्ट छिड़ककर रेशमी हवाओं पर तैरने लगती। दर्पण देखती तो छाया महक उठती। भाई श्रृंगार करते देखते, तो मुसकराकर कहते, ‘‘ओह, लॅवली-लॅवली !’’ और में सकुचा जाती।
उस रोज भी दिवाकर आया, क़ागजों का बड़ा-सा पुलिन्दा बग़ल में दबाये बैठा था। डैडी और ममी उसे बहुत चाहते थे। ममी ने आवाज़ लगायी, ‘‘दिवाकर आया है !’’ बिन्दी लगाते-लगाते मेरा हाथ काँप जाता। उसे मेरे माथे पर दीपक की लौ-जैसी रेखा कितनी पसन्द है ! मैंने साड़ी का पल्ला ठीक किया, उसकी निचाई ठीक की और उतावली-सी नीचे उतर आयी। दिवाकर ने मुसकराकर मेरी ओर देखा और मैं सपनो में डूब गयी। बड़ा आदर्शवादी है। वह धीमे से आता था। सुरुचिपूर्ण पर सादा पहनावा। बड़ी गहरी अथाह आँखें; माथे को चूमती काली-कजरारी लटें। मस्तक पर दृढ़ती की लकीरें और होंठों में छुपी हुई विनम्र-निर्मल मुसकान। सिगरेट बहुत पीता था, इसीलिए उसके साँवले रंग में भी होंठों की कालिख दिख जाती थी।
वह कुछ पेसोपेश में पड़ा हुआ था, जैसे आने का कोई कारण न खोज पा रहा हो। कुछ अजीब-सी प्यारी शर्म, और उसके आने का मन्तव्य खुल जाने की लज्जा, और उस निरर्थकता पर पश्चात्ताप करता हुआ उसका भाव ! वह रोज़ प्रथम क्षणों में ऐसा ही परेशान दिखता। यह उसका स्वभाव है। मैं तो अभ्यस्त हो चुकी हूँ। इन्हीं असमंजस के क्षणों में यदि कोई मज़ाक भी कर बैठे कि दिवाकर कैसे आये; तो वह शर्तिया भाग जाये। अपने आप के औचित्य को वह रोज़ ही साबित करता था, ‘‘इधर से जा रहा था, सोचा, देखता चलूँ...’—इतना कह लेने के बाद वह सामान्य हो जाता था। फिर हँसने-बोलने लगता। शब्दों का तो जादूगर था। ममी भी बड़ी बातूनी हैं और डैडी भी कम नहीं।
न जाने उस रोज़ क्या हुआ। दिवाकर एकाएक बातों में गम्भीर हो गया। वैसे वह सदैव सीमाओं पर ही रहता था। निश्चित रुचियों और मनोभावों का आदमी था। वह जब बोलता तो लगता कि उसकी आत्मा बोल रही है, प्यार या घृणा कर रही है, ग़लत या सही समझ रही है। संशय और अनिश्चितता के लिए वहाँ जगह नहीं थी। इसीलिए अन्त में वह जीत जाता। उसकी बातें सभी को सोचने के लिए मजबूर कर देतीं; चकित कर जाती थीं। मैं उत्सुकता से सुनती। बड़ा अव्यक्त सुख मिलता था।
उसके जाने के बाद घर में उसका प्रभाव छाया रहता। ममी बात-बात में उसकी मिसालें देतीं, ‘‘दिवाकर को देखो, जितना पढ़ता जाता है, उतना ही विनीत होता जाता है। तुम लोग चार अक्षर पढ़कर घमण्डी होते जा रहे हो। कैसे क़ायदे से बात करता है...’’
एक रोज़ मैंने बड़े संकोच से उससे कह दिया था, ‘‘सबके सामने तुम्हारे साथ बैठते हुए मुझे न जाने कैसा लगता है। तुम भोले बन जाते हो, जैसे कुछ जानते ही नहीं !’’
‘‘मैं क्या जानूँ !’’ कहते हुए दिवाकर मुसकरा दिया था।
उसकी न जाने कितनी स्मृतियाँ हैं।
अपने काग़ज़ के बण्डल को दिवाकर ने मेज़ पर रखा। डैडी चलते-चलते कोई-न-कोई बात छेड़ देते थे। ममी और दिवाकर उलझे रह जाते। ममी दिवाकर से बोलीं, ‘‘क्यों दिवाकर, कम्पटीशन में बैठने का इरादा नहीं है ?’’
‘‘क्या रखा है उनमें, कम-से-कम मेरे लिए तो नहीं है। सब अफ़सर हो जाएँगे तो ब़ाकी काम कौन करेगा।’’ दिवाकर ने कहा।
सुनकर डैडी बोल पड़े, ‘‘भाई, बग़ैर सिक्योरिटी के जीने का कोई मतलब नहीं है। रोज कुआँ खोदना अक़्लमंदी नहीं है। तुम्हारी बात और है, पर दूसरे युवकों की ज़िन्दगियाँ बरबाद होते देखकर अफ़सोस भी होता है, ग़ुस्सा भी आता है।...बुरी तरह भटक रहे हैं। यह नहीं जानते कि क्या करें ? लापरवाही और वक़्त की बरबादी, बस यही उनका काम है...’’
सुनकर दिवाकर न जाने कैसा हो आया। वह आक्षेपों को बरदाश्त नहीं कर पाता था। उसका क्षण-भर पहले का संकोच बड़े विनत साहस से भर गया। बोला, ‘‘नौजवानों की फ़िक्र आपको नहीं होनी चाहिए।
उनके प्रति जो रुख आप लोगों, यानी पुरानी पीढ़ी का है, वह कितना निकम्मा और बोदा है, यह ख़ुद आप भी जानते हैं। बड़े ग़लत पैमाने बना रखे हैं आप लोगों ने। आप युवकों को उनकी पोशाक से जाँचते हैं। फ़लाँ यह पहनता था, इसलिए वह ज़िन्दगी में क्या कर सकता है ! युवकों के उन्हीं क्षणों को आप पकड़ते हैं, जिन्हें तरह दे देना चाहिए। अपनी सार्थकता के लिए आज का नौजवान जिस मानसिक संघर्ष से गुज़र रहा है, वह कितना चिन्तित है यह आपने नहीं देखा। आपने सड़क से गुज़रते-गुज़रते, होटलों से आते उनके ठहाके सुने हैं, लेकिन यह कभी देखने की कोशिश नहीं की कि उन ठहाकों के बाद एकाएक उनकी मेज़ों पर कैसी उदासी छा जाती है ! कितनी ईमानदारी से वे सोचते हुए उठते हैं और छोटे-बड़े कामों में लग जाते हैं। उनकी हँसी आपको आवारागर्दी-भरी लगती है। उनका सहज अल्हड़पन सभ्यता की सीमा के बाहर दिखाई पड़ता है।
उनका हँसना-बोलना, चलना-फिरना, यहाँ तक कि उनकी रुचियों और मनोभावनाओं से आप चिढ़ते हैं, उदारता से बरदाश्त नहीं कर पाते। यह कमी उनकी नहीं, आपकी है। यह आपकी पीढ़ी का दृष्टि दोष है। आप लोग सिर्फ़ अपने जीवन का नमूना पेश करते हैं, अपने विचारों को अन्तिम मानते हैं, उन्हीं में उसकी शक्ति, सपने और कल्पना को क़ैद कर लेना चाहते हैं...’’—वह धाराप्रवाह बोलता गया। ममी आश्चर्य से ताक रही थीं और डैडी हतप्रभ थे। मेरा मन हुसल आया। दिवाकर के चेहरे से रोशनी फूट रही थी। वह हर समस्या को नये दृष्टिकोण से देखता था। बड़ा अजीब विश्वास था उसका। उसकी बात हमेशा नवीन होती। एक ही बात को तरह-तरह से देखता और जिस पहलू को उभारकर रख देता, वही उस समस्या का मुख्य पहलू बन जाता। उसके शब्दों में जादू था। इस जादू में मैं खो जाती थी। उसके पास लहराते जीवन और विचारों के अपार सागर में डूब-डूब जाती।
वह मुझसे कहा करता था, ‘‘मीना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें क्या दे पाऊँगा ?’’
लेकिन मैं उसके आत्मविश्वास से परिचित थी। वह कहीं बाहर जाता तो पोथियाँ की पोथिया रँगकर लाता। ममी देखकर कहती थीं, ‘बड़ी मेहनत करता है दिवाकर।’ मुझे लगता, यह श्रेय मुझे मिल रहा है।
पर इस समय ममी की आँखों में वैसी प्रशंसा नहीं थी।
डैडी असली बात स्वीकार करते हुए बोले, ‘‘हाँ, यह हमारी पीढ़ी की कमी हो सकती है, लेकिन इससे जीवन की सुरक्षा का मसला हल नहीं होता।’
दिवाकर धीरे से मुसकराया। अपनी सहज नम्रता को पकड़ते हुए ममी की ओर देखकर बोला, ‘‘आप भी क्या ऐसा ही सोचती हैं ?’’ फिर उसने डैडी की ओर देखा और कहने लगा, ‘‘ग़ुलामी ने हमारी सम्भावनाएँ अभी तक रोक रखी थीं। हम ठहरे हुए थे। जीवन की सुरक्षा और गतिशीलता बहुत दूर तक एक साथ नहीं चल सकतीं। सुरक्षा केवल वे चाहते हैं जो हताश हैं; जिनका विश्वास अपने पर से टूट चुका है। आप ही हैं; यदि आपको अपनी कुशलता पर यकीन न होता तो क्या आप इतने सफल डॉक्टर बन पाते ? लेकिन आप खुद अपनी कुशलता पर विश्वास रखते हुए भी दूसरे की शक्ति में अविश्वास करते हैं, इसीलिए आपको हर तरफ पतन, दुराचार और अँधेरा दिखाई पड़ता है। नयी पीढ़ी हमेशा असन्तोष का विषय रही है, पर वह कुछ ऐसा करती आयी है, जो पिछली नहीं कर पायी और दुनिया बढ़ती गयी.....’’
‘‘भाई, ये बातें अपनी समझ से बाहर हैं,’’ ममी बोलीं, ‘‘अब यही देख लो ये रोज़ रट लगाए रहते हैं कि दवाइयों में मिलावट होने लगी। यह पतन नहीं है ?’’
‘‘और जो नयी दवाइयाँ रोज़ खोजी जा रही हैं, यह प्रगति नहीं है क्या ?’’ दिवाकर बोला, ‘‘जिस पतन की बात आप कर रही हैं, वह सब हमें पैसे की संस्कृति ने दिया है, इसी सुरक्षा वाली भावना ने। इसी ने हमें स्वार्थी बनाया है। यह आखिर है क्या ? केवल पैसा ! और आप किस बात की सुरक्षा चाहते हैं ? जीवन की सद्भावनाओं से विकल होकर कोई इन बुराइयों को नहीं देखता। कुछ लोग चार सौ बीसी से धनवान बन बैठे हैं, इसलिए उनसे, उनकी सुविधाओं से जो ईर्ष्या मन में उपजी है, वही यह कहलवा रही है। यह ग़लत है। लेकिन ‘व्यक्तियों’ के समाज में हमेशा ऐसा ही होता है, ‘समाज के व्यक्तियों में’ नहीं। ‘व्यक्तियों का समाज’ भी बड़े मज़ेदार कल्पना है ! वह व्यक्ति-विशेष दिमाग़ की उपज है, जो अपने हितों के लिए अपने आस-पास समाज जोड़ते हैं।
लेकिन ‘समाज का व्यक्ति’ स्वतंत्र होते हुए भी निराकार होता है, स्वतंत्रता ही उसका व्यक्तित्व है, इसीलिए समाज प्रगति करता है। इसमें व्यक्ति-व्यक्ति की होड़ नहीं होती। सामूहिक विकास होता है। यह आपकी छोटी-छोटी पसन्दें, ये आपके निजी पैमाने, आपकी अनूठी रुचियाँ...ज़रा सोचकर देखिए, कितनी थोथी हैं ! इन्हीं के लिए हम जियें और मरें ? इन्हीं ने हमें बड़े कामों की ओर उदासीन कर रखा है। इनके लिए हमारे पास समय कहाँ है....’’
न जाने क्या हो गया था दिवाकर को। मैं सोच रही थी कि अभी वह सारी बातों का रुख पलट देगा और सबके चेहरे पहले की तरह मुसकराने लगेंगे। वह कोई मज़ेदार घटना सुनाएगा और ममी कहेंगी, ‘‘कहानियाँ तो कोई इससे सुने !’’ पर सहसा ममी ने कहा, ‘‘लेकिन जिनके पास समय है, साधन है, वे क्यों न अपनी रुचियों का विकास करें, उन्हें हक है...’’
‘‘वह समय और साधन उनके नहीं हैं,’’ दिवाकर बोला, ‘‘अगर हर आदमी अकेला जीता होता तो क्या ये सुविधाएँ उनके पास होतीं ? हम आज भी जंगलों में जानवरों की तरह भटकते होते ! इन अतिरिक्त सुविधाओं के लिए सभी ने जाने-अनजाने हाथ बँटाया है, यह उन्होंने पैदा की हैं। जो उनके लिए तरस रहे हैं। व्यक्ति इत्र छिड़ककर फूल सूँघता हुआ इन फटेहालों के बीच से निरपेक्ष होकर गुज़र सकता है, आदमी नहीं। व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, आदमी स्वतन्त्रता चाहता है। सुरक्षा और स्वतन्त्रता में बड़ा अन्तर है। स्वतन्त्रता एक का नहीं, सबका अधिकार है !’’
डैडी ऊबने लगे थे। ममी ने चाय के लिए आवाज लगाई। मैं तो सचमुच खो गई थी। मन होता था, सिल्क के कपड़े उतार फेंकूँ। उस दिन पहली बार मुझे इस खोखली जिन्दगी के अतिशय बनाव-श्रृंगार, तौर-तरीकों, हाव-भावों में अरुचि हुई थी। जीवन की अर्थहीनता और व्यर्थ नाटकीयता तथा बनावट से असंतोष हुआ था। क्या मैं इनसे बड़ी बातों के लिए नहीं जी सकती ? दिन-भर केवल यह देह क्यों सजाती हूँ ? शीशे में घण्टों परछाईं से बातें क्यों करती हूँ ? न जाने कैसी श्रद्धा उपजी थी उस दिन ! पर डैडी और ममी के चेहरे उतरे हुए थे, जैसे उनके जीवन-भर के श्रम को किसी ने व्यर्थ कर दिया हो।
चाय आयी और हम पीने बैठ गये। इतने में भाई साहब और जितेन आ गये। वातावरण हलका हुआ। जितेन ने मुसकराते हुए कहा, ‘‘मैं बता सकता हूँ कि इस वक़्त कौन-सा सेण्ट महक रहा है !’’ कहते हुए उसने उड़ती नज़र सब पर डालकर मेरी ओर देखा और खिलखिलाकर हँसते हुए बोला, ‘‘चम्पा !’’
ममी ने चाय पीते हुए प्रशंसा से भरकर कहा, ‘‘जितेन बड़ा तेज है।’’
सबकी नजरों में प्रशंसा झाँकने लगी।
जितेन ने डैडी के पैरों की ओर देखते हुए कहा, ‘‘अंकिल, अब आप यह पतली टो का जूता पहनना छोड़ दीजिए !’’
‘‘मैंने ब्राड-कप-शेप बनवाया है !’’—भाई साहब ने कहा।
बेदम मछलियाँ फिर पानी में पहुँच गयीं।...जू में नया चीता आया है।...हिन्दी पिक्चर्स बेकार होती हैं। ....इस बार भी डर्बी की प्राइज किसी अमेरिकी व्यापारी को मिली है।...
दिवाकर फिर संकुचित होने लगा। कैसे बैठे हो, दिवाकर ! कोई पूछ लेता, तो शर्तिया उठकर भाग जाता। जितेन की बातों से मेरा मन ऊबने लगा। मुझे लगा कि दिवाकर मेरा उठ जाना पसन्द करेगा। मैं उठ गयी।
उस दिन से अजीब कशमकश रहती। मेरा मन होता कि सबको छोड़कर दिवाकर का हाथ पकड़ लूँ और कहूँ, चाहे जहाँ ले चलो। मैं स्वतन्त्र हूँ। तुम्हें अपना मान चुकी हूँ। तुम्हारी आग मुझे आकर्षित करती है। सचमुच जीवन में सुरक्षित क्या है ? तुम अपनी मुक्ति में मुझे भी बाँध लो। मेरे जीवन का छूटा हुआ सत्य मुझे दे दो !..
एक रात सपना देखा। दिवाकर के साथ न जाने कहाँ-कहाँ घूम रही हूँ। वह जहाँ भी जाता है, लोग प्यार से उसे घेर लेते हैं। वापसी पर वह बहुत थक गया है। पर रात गए तक वह मेज़ पर झुका घण्टों बैठ लिखता रहा। मैंने पीछे से जाकर उसके छितराए हुए बालों को चूम लिया। फिर उसकी बाँहों के घेरे। नहीं....नहीं...इसे पूरा कर लो, दिवाकर...और देर बाद थक कर वह मेरी गोद में पड़ा निश्शंक, निर्द्वन्द्व सो रहा है। आँखें खुलीं तो कुछ भी नहीं था। मैं निपट अकेली थी।
न जाने वह क्या-क्या बताया करता था। एक दिन बोला था, ‘‘अपनी ज़िंदगी जियो मीना ! तुम्हारा सौंदर्य के प्रति अनुराग मुझे अच्छा लगता है, जहाँ तक वह तुम्हारा है। लेकिन जब तुम लोग नक़ल करते हो तो बौने लगते हो। तुम जीवनियाँ पढ़ती हो। वे इसलिए आकर्षिक करती हैं कि वे उन लोगों की अपनी हैं। राहुल की जीवनी पढ़कर कितनों ने विद्रोह नहीं किया होगा ! भागे होंगे। लेकिन किसी का नाम सुनाई पड़ता है ! कोई कुछ कर पाया ? अपनी मौलिकता सबसे बड़ी निधि है। उन जीवनियों की सतत प्यास को पहचानों ! यह तुम्हारा फूलों का प्यार, यह हर शाम की एक-सी मुस्कान, पपी को गोद में लेकर सहलाना और रटे हुए वाक्यों की बौछार, यह एकसरता धीरे-धीरे तुम्हें निर्जीव बना देगी...’’
मैं बहुत सोचती उन बातों पर, और मुझे लगता कि मैं दिवाकर को बेहद चाहने लगी हूँ। लेकिन उस दिन के बाद में उसकी आलोचना होने लगी। कभी दिवाकर का जिक्र आता, तो ममी कहतीं, ‘‘दिवाकर जान-बूझकर अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है। उसका यह ऊट-पटाँग सोचना और लिखना-लिखाना किस काम आयेंगे ! कल ठोकरें खायेगा, तब दिमाग़ रास्ते पर आ जायेगा।’’
मैं सुनती तो ठिठक जाती। पहले ममी की जबान उसकी तारीफ़ करते नहीं थकती थी। आखिर उस दिन उसने ऐसा क्या-कुछ कह दिया, जो सबका दिमाग़ पलट गया। उसकी बुराई होती तो मुझे चुभती।
उस दिन के बाद दिवाकर का स्वागत रूखा होने लगा। डैडी धीरे से मुसकराकर उठ जाते। ममी इधर-उधर की बातें करके जैसे टालने लगीं। उसके जाते ही हजारों बातें शुरू हो जातीं, इन लेखकों-सुधारकों का कोई ठिकाना है ? न जाने क्यों, डैडी और ममी दिवाकर को लेखक पुकारते थे और सुधारकों से उसकी तुलना करते थे !.....ये लोग तो मिराकी होते हैं। ग़रीबों की हिमायत करते हैं और उन्हीं का ख़ून चूसते हैं ! अच्छा-ख़ासा तेज़ लड़का था। किसी तरफ़ लगता तो चमक जाता। नेता हो गया है। ऊटपटाँग कपड़े पहनता है....’
धीरे-धीरे उसका आना कम होता गया। जितेन अब भी आता था। दिवाकर की ख़बर मिलनी भी कम हो गयी। मुझे उसकी याद आती थी। उसके साथ बिताये क्षण याद आते थे। पर जो करना चाहती थी, वह नहीं हो पाता था। कभी वह आता तो सबकी नज़रें मेरी तरफ़ रहतीं। उसके साथ उठने-बैठने, घूमने-घामने पर अदृश्य पाबंदी-सी लगी दिखाई देती। वह भी न जाने कैसा हो गया था। जिन बातों से डैडी और ममी को चिढ़ होती थी, वही अदबदाकर करता। जान-बूझकर खद्दर पहन आता। कलीदार कुरता पहनकर अजीब तरह से बातें करता। मैं उसके लिखे पत्रों के खोलकर पुरानी बातें याद करती। समय-समय पर उसकी भाव-भंगिमाएँ याद करती। पर एक दिन ममी ने बहुत अपनेपन से कहा, ‘‘मीनू, तू नाहक उलझी रहती है। ज़िन्दगी को इस तरह नहीं लेते। कोई अपने को योग्य साबित न कर सके, इसमें उसकी ग़लती है, तेरी नहीं।’’
और एक दिन दिवाकर मुझे अकस्मात् अशोक रोड पर मिल गया। कहने लगा, कहीं बाहर जा रहा है। मैं जाने क्यों उससे अधिक बात नहीं कर पायी। घर पहुँचने की जल्दी थी। घर आते ही जितेन इन्तज़ार करते मिला। ममी और डैडी ड्राइंगरूम में ही बैठे थे। मुझे देखते ही जितेन बोला, ‘‘चलिए आंटी, मीना भी आ गयी, अब प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता।’’ और उस रात हम सिनेमा चले गये। जितेन मुझे चारों ओर से ऐसे घेरे रहा, जैसे मैं उसकी हूँ। बड़ी अनूठी अनुभूति हुई उस रात। जितेन रास्ते-भर पिक्चर की तारीफ़ करता रहा, विशेषकर इटैलियन नर्तकी की। उसकी चेष्टाएँ अनदेखे ही बढ़ती गयीं। ममी की ओर संकोच से मैंने देखा। वह असंतुष्ट थीं। उनके व्यवहार में छूट और इस ओर से लापरवाही थी।
दिन बीतते रहे। दिवाकर कहीं-न-कहीं मिलता रहा। कभी-कभी मुझे यह भी लगता कि उसका यह मिलना आकस्मिक नहीं होता। एक रोज़ मैं ऊपर वाले कमरे में थी। सड़क पर दिवाकर का भ्रम हुआ, कुछ देर बाद फिर भ्रम हुआ, शायद वह वापस जा रहा था। मैं उतरकर नीचे लॉन में आ गयी। कुछ देर बाद वह फिर गुज़रा। उसने उड़ती हुई निगाह मेरी ओर डाली। मुझे देखा और निकल गया। मैं इन्तज़ार करती रही कि वह अब वापस आये तो रोक लूँगी, पर वह नहीं आया।
और इसके बाद वह दिन...
शाम थी। सभी लोग बैठे गपशप कर रहे थे। जितेन के क़हक़हों से कमरा गूँज रहा था। वह कह रहा था, ‘‘हिन्दुस्तान की इमारतों का क्या देखना ? इमारतें देखना है तो अमेरिका की देखिए। आरामदेह और खूबसूरत ! सादगी और खूबसूरती में अमेरिका मॉडल का जोड़ नहीं ! मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि जिसने अमेरिका नहीं देखा, वह इंजीनियर हो ही नहीं सकता !’’
‘‘इसमें क्या शक !’’ भाई साहब बोले।
‘‘ग़नीमत है कि शर्माजी यहाँ नहीं हैं, नहीं तो अमेरिका की इमारतों का सम्बन्ध वेदों से जुड़ गया होता !’’ जितेन ने कहा और हम सभी हँस पड़े। मैं क्यों हँसी, शायद जितेन के कारण।
तभी भाई साहब ने उसी मज़ाक़ के दौरान कहा, ‘‘श्री दिवाकर जी हिन्दी-प्रचारक होकर आसाम चले गये हैं।’’
श्री और जी सुनकर जितेन हँस पड़ा। बोला, ‘‘आसाम के जंगलों में ! आखिर हिन्दी संस्किरित की बेटी है !’’
सुनकर डैडी मुसकरा दिये।
मुझे एकाएक कुछ बुरा-सा लगा, यह सोचकर कि वह कितनी दूर चला गया। अकेला गया होगा। और उसके बाद दिवाकर का कोई समाचार नहीं मिला।
आज सोचती हूँ तो मन भर-भर आता है। कितने बड़े झूठ और प्रवंचना में हम साँस ले रहे हैं। सुरक्षा, काहे की ? जीवन की ! और यह पैसा और पद ? क्या यही जीवन की सम्पूर्ण प्राप्ति है ? मुझे घृणा होती है। क्या यही जीने का मतलब है और क्या यही आवश्यक है कि एक पुरुष अपनी प्रतिष्ठा की बाँहों में घेरकर भौतिक सुविधाओं से भर दे, जीवन की यह झूठी सुरक्षा दे दे ? प्यार करे ? शारीरिक सम्बन्ध रखे, क्लब और होटलों में ले जाये, पार्टियों में पत्नी को अप्सरा बनाकर औरों की ईर्ष्या में सुख पाये ?
यही हमारा जीवन है, स्वतंत्रता और सभ्यता का जीवन। यह नारी स्वतंत्रता हाथी के दाँत हैं, जिन्हें हर घराना खूबसूरती के लिए लगाए हुए है ! सारी लड़कियाँ स्वतंत्र हैं, वे प्यार कर सकती हैं, घृणा कर सकती हैं, लेकिन जो चाहती हैं वह नहीं कर सकतीं। वे शादी से पहले एकान्त स्थानों में घूम सकती हैं, प्रेम का हर नाटक कर सकती हैं, यह आज़ादी नहीं तो क्या ? मैं भी घूमी हूँ। युवकों के संसर्ग में आयी हूँ। प्यार छिपा-छिपाकर नहीं, दिखा-दिखाकर किया है और इस बात पर विश्वास करती थी कि अन्तिम और गहनतम प्रेम वही होता है, जो अन्त में हो।
लेकिन वे दिन आज याद आते हैं। उन्हें कैसे भूल जाऊँ ? शाम को आने वाले हर परिचित और रिश्तेदार का स्वागत मैं मुसकराकर करती थी। हमारे घरों की शामें इसीलिए होती हैं। सच, तब मुझे यह अच्छा लगता था। विशेषकर इसलिए कि दिवाकर आता था। शाम होते ही डैडी क्लीनिक के लिए तैयार होने लगते। ममी ऐसे तैयार होती, जैसे यह सब करना स्वास्थ्य और ताज़गी के लिए आवश्यक हो। मेरी नसों में बिजली दौड़ जाती। शाम ही तो सचमुच मेरे लिए होती थी। मैं साड़ी बदलती, उसका रंग चुनती, मौसम देखकर रिबनों के रंग बदलती। आँखों में लंबी सलाई से काजल डालती, फिर ढेर-सा सेण्ट छिड़ककर रेशमी हवाओं पर तैरने लगती। दर्पण देखती तो छाया महक उठती। भाई श्रृंगार करते देखते, तो मुसकराकर कहते, ‘‘ओह, लॅवली-लॅवली !’’ और में सकुचा जाती।
उस रोज भी दिवाकर आया, क़ागजों का बड़ा-सा पुलिन्दा बग़ल में दबाये बैठा था। डैडी और ममी उसे बहुत चाहते थे। ममी ने आवाज़ लगायी, ‘‘दिवाकर आया है !’’ बिन्दी लगाते-लगाते मेरा हाथ काँप जाता। उसे मेरे माथे पर दीपक की लौ-जैसी रेखा कितनी पसन्द है ! मैंने साड़ी का पल्ला ठीक किया, उसकी निचाई ठीक की और उतावली-सी नीचे उतर आयी। दिवाकर ने मुसकराकर मेरी ओर देखा और मैं सपनो में डूब गयी। बड़ा आदर्शवादी है। वह धीमे से आता था। सुरुचिपूर्ण पर सादा पहनावा। बड़ी गहरी अथाह आँखें; माथे को चूमती काली-कजरारी लटें। मस्तक पर दृढ़ती की लकीरें और होंठों में छुपी हुई विनम्र-निर्मल मुसकान। सिगरेट बहुत पीता था, इसीलिए उसके साँवले रंग में भी होंठों की कालिख दिख जाती थी।
वह कुछ पेसोपेश में पड़ा हुआ था, जैसे आने का कोई कारण न खोज पा रहा हो। कुछ अजीब-सी प्यारी शर्म, और उसके आने का मन्तव्य खुल जाने की लज्जा, और उस निरर्थकता पर पश्चात्ताप करता हुआ उसका भाव ! वह रोज़ प्रथम क्षणों में ऐसा ही परेशान दिखता। यह उसका स्वभाव है। मैं तो अभ्यस्त हो चुकी हूँ। इन्हीं असमंजस के क्षणों में यदि कोई मज़ाक भी कर बैठे कि दिवाकर कैसे आये; तो वह शर्तिया भाग जाये। अपने आप के औचित्य को वह रोज़ ही साबित करता था, ‘‘इधर से जा रहा था, सोचा, देखता चलूँ...’—इतना कह लेने के बाद वह सामान्य हो जाता था। फिर हँसने-बोलने लगता। शब्दों का तो जादूगर था। ममी भी बड़ी बातूनी हैं और डैडी भी कम नहीं।
न जाने उस रोज़ क्या हुआ। दिवाकर एकाएक बातों में गम्भीर हो गया। वैसे वह सदैव सीमाओं पर ही रहता था। निश्चित रुचियों और मनोभावों का आदमी था। वह जब बोलता तो लगता कि उसकी आत्मा बोल रही है, प्यार या घृणा कर रही है, ग़लत या सही समझ रही है। संशय और अनिश्चितता के लिए वहाँ जगह नहीं थी। इसीलिए अन्त में वह जीत जाता। उसकी बातें सभी को सोचने के लिए मजबूर कर देतीं; चकित कर जाती थीं। मैं उत्सुकता से सुनती। बड़ा अव्यक्त सुख मिलता था।
उसके जाने के बाद घर में उसका प्रभाव छाया रहता। ममी बात-बात में उसकी मिसालें देतीं, ‘‘दिवाकर को देखो, जितना पढ़ता जाता है, उतना ही विनीत होता जाता है। तुम लोग चार अक्षर पढ़कर घमण्डी होते जा रहे हो। कैसे क़ायदे से बात करता है...’’
एक रोज़ मैंने बड़े संकोच से उससे कह दिया था, ‘‘सबके सामने तुम्हारे साथ बैठते हुए मुझे न जाने कैसा लगता है। तुम भोले बन जाते हो, जैसे कुछ जानते ही नहीं !’’
‘‘मैं क्या जानूँ !’’ कहते हुए दिवाकर मुसकरा दिया था।
उसकी न जाने कितनी स्मृतियाँ हैं।
अपने काग़ज़ के बण्डल को दिवाकर ने मेज़ पर रखा। डैडी चलते-चलते कोई-न-कोई बात छेड़ देते थे। ममी और दिवाकर उलझे रह जाते। ममी दिवाकर से बोलीं, ‘‘क्यों दिवाकर, कम्पटीशन में बैठने का इरादा नहीं है ?’’
‘‘क्या रखा है उनमें, कम-से-कम मेरे लिए तो नहीं है। सब अफ़सर हो जाएँगे तो ब़ाकी काम कौन करेगा।’’ दिवाकर ने कहा।
सुनकर डैडी बोल पड़े, ‘‘भाई, बग़ैर सिक्योरिटी के जीने का कोई मतलब नहीं है। रोज कुआँ खोदना अक़्लमंदी नहीं है। तुम्हारी बात और है, पर दूसरे युवकों की ज़िन्दगियाँ बरबाद होते देखकर अफ़सोस भी होता है, ग़ुस्सा भी आता है।...बुरी तरह भटक रहे हैं। यह नहीं जानते कि क्या करें ? लापरवाही और वक़्त की बरबादी, बस यही उनका काम है...’’
सुनकर दिवाकर न जाने कैसा हो आया। वह आक्षेपों को बरदाश्त नहीं कर पाता था। उसका क्षण-भर पहले का संकोच बड़े विनत साहस से भर गया। बोला, ‘‘नौजवानों की फ़िक्र आपको नहीं होनी चाहिए।
उनके प्रति जो रुख आप लोगों, यानी पुरानी पीढ़ी का है, वह कितना निकम्मा और बोदा है, यह ख़ुद आप भी जानते हैं। बड़े ग़लत पैमाने बना रखे हैं आप लोगों ने। आप युवकों को उनकी पोशाक से जाँचते हैं। फ़लाँ यह पहनता था, इसलिए वह ज़िन्दगी में क्या कर सकता है ! युवकों के उन्हीं क्षणों को आप पकड़ते हैं, जिन्हें तरह दे देना चाहिए। अपनी सार्थकता के लिए आज का नौजवान जिस मानसिक संघर्ष से गुज़र रहा है, वह कितना चिन्तित है यह आपने नहीं देखा। आपने सड़क से गुज़रते-गुज़रते, होटलों से आते उनके ठहाके सुने हैं, लेकिन यह कभी देखने की कोशिश नहीं की कि उन ठहाकों के बाद एकाएक उनकी मेज़ों पर कैसी उदासी छा जाती है ! कितनी ईमानदारी से वे सोचते हुए उठते हैं और छोटे-बड़े कामों में लग जाते हैं। उनकी हँसी आपको आवारागर्दी-भरी लगती है। उनका सहज अल्हड़पन सभ्यता की सीमा के बाहर दिखाई पड़ता है।
उनका हँसना-बोलना, चलना-फिरना, यहाँ तक कि उनकी रुचियों और मनोभावनाओं से आप चिढ़ते हैं, उदारता से बरदाश्त नहीं कर पाते। यह कमी उनकी नहीं, आपकी है। यह आपकी पीढ़ी का दृष्टि दोष है। आप लोग सिर्फ़ अपने जीवन का नमूना पेश करते हैं, अपने विचारों को अन्तिम मानते हैं, उन्हीं में उसकी शक्ति, सपने और कल्पना को क़ैद कर लेना चाहते हैं...’’—वह धाराप्रवाह बोलता गया। ममी आश्चर्य से ताक रही थीं और डैडी हतप्रभ थे। मेरा मन हुसल आया। दिवाकर के चेहरे से रोशनी फूट रही थी। वह हर समस्या को नये दृष्टिकोण से देखता था। बड़ा अजीब विश्वास था उसका। उसकी बात हमेशा नवीन होती। एक ही बात को तरह-तरह से देखता और जिस पहलू को उभारकर रख देता, वही उस समस्या का मुख्य पहलू बन जाता। उसके शब्दों में जादू था। इस जादू में मैं खो जाती थी। उसके पास लहराते जीवन और विचारों के अपार सागर में डूब-डूब जाती।
वह मुझसे कहा करता था, ‘‘मीना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें क्या दे पाऊँगा ?’’
लेकिन मैं उसके आत्मविश्वास से परिचित थी। वह कहीं बाहर जाता तो पोथियाँ की पोथिया रँगकर लाता। ममी देखकर कहती थीं, ‘बड़ी मेहनत करता है दिवाकर।’ मुझे लगता, यह श्रेय मुझे मिल रहा है।
पर इस समय ममी की आँखों में वैसी प्रशंसा नहीं थी।
डैडी असली बात स्वीकार करते हुए बोले, ‘‘हाँ, यह हमारी पीढ़ी की कमी हो सकती है, लेकिन इससे जीवन की सुरक्षा का मसला हल नहीं होता।’
दिवाकर धीरे से मुसकराया। अपनी सहज नम्रता को पकड़ते हुए ममी की ओर देखकर बोला, ‘‘आप भी क्या ऐसा ही सोचती हैं ?’’ फिर उसने डैडी की ओर देखा और कहने लगा, ‘‘ग़ुलामी ने हमारी सम्भावनाएँ अभी तक रोक रखी थीं। हम ठहरे हुए थे। जीवन की सुरक्षा और गतिशीलता बहुत दूर तक एक साथ नहीं चल सकतीं। सुरक्षा केवल वे चाहते हैं जो हताश हैं; जिनका विश्वास अपने पर से टूट चुका है। आप ही हैं; यदि आपको अपनी कुशलता पर यकीन न होता तो क्या आप इतने सफल डॉक्टर बन पाते ? लेकिन आप खुद अपनी कुशलता पर विश्वास रखते हुए भी दूसरे की शक्ति में अविश्वास करते हैं, इसीलिए आपको हर तरफ पतन, दुराचार और अँधेरा दिखाई पड़ता है। नयी पीढ़ी हमेशा असन्तोष का विषय रही है, पर वह कुछ ऐसा करती आयी है, जो पिछली नहीं कर पायी और दुनिया बढ़ती गयी.....’’
‘‘भाई, ये बातें अपनी समझ से बाहर हैं,’’ ममी बोलीं, ‘‘अब यही देख लो ये रोज़ रट लगाए रहते हैं कि दवाइयों में मिलावट होने लगी। यह पतन नहीं है ?’’
‘‘और जो नयी दवाइयाँ रोज़ खोजी जा रही हैं, यह प्रगति नहीं है क्या ?’’ दिवाकर बोला, ‘‘जिस पतन की बात आप कर रही हैं, वह सब हमें पैसे की संस्कृति ने दिया है, इसी सुरक्षा वाली भावना ने। इसी ने हमें स्वार्थी बनाया है। यह आखिर है क्या ? केवल पैसा ! और आप किस बात की सुरक्षा चाहते हैं ? जीवन की सद्भावनाओं से विकल होकर कोई इन बुराइयों को नहीं देखता। कुछ लोग चार सौ बीसी से धनवान बन बैठे हैं, इसलिए उनसे, उनकी सुविधाओं से जो ईर्ष्या मन में उपजी है, वही यह कहलवा रही है। यह ग़लत है। लेकिन ‘व्यक्तियों’ के समाज में हमेशा ऐसा ही होता है, ‘समाज के व्यक्तियों में’ नहीं। ‘व्यक्तियों का समाज’ भी बड़े मज़ेदार कल्पना है ! वह व्यक्ति-विशेष दिमाग़ की उपज है, जो अपने हितों के लिए अपने आस-पास समाज जोड़ते हैं।
लेकिन ‘समाज का व्यक्ति’ स्वतंत्र होते हुए भी निराकार होता है, स्वतंत्रता ही उसका व्यक्तित्व है, इसीलिए समाज प्रगति करता है। इसमें व्यक्ति-व्यक्ति की होड़ नहीं होती। सामूहिक विकास होता है। यह आपकी छोटी-छोटी पसन्दें, ये आपके निजी पैमाने, आपकी अनूठी रुचियाँ...ज़रा सोचकर देखिए, कितनी थोथी हैं ! इन्हीं के लिए हम जियें और मरें ? इन्हीं ने हमें बड़े कामों की ओर उदासीन कर रखा है। इनके लिए हमारे पास समय कहाँ है....’’
न जाने क्या हो गया था दिवाकर को। मैं सोच रही थी कि अभी वह सारी बातों का रुख पलट देगा और सबके चेहरे पहले की तरह मुसकराने लगेंगे। वह कोई मज़ेदार घटना सुनाएगा और ममी कहेंगी, ‘‘कहानियाँ तो कोई इससे सुने !’’ पर सहसा ममी ने कहा, ‘‘लेकिन जिनके पास समय है, साधन है, वे क्यों न अपनी रुचियों का विकास करें, उन्हें हक है...’’
‘‘वह समय और साधन उनके नहीं हैं,’’ दिवाकर बोला, ‘‘अगर हर आदमी अकेला जीता होता तो क्या ये सुविधाएँ उनके पास होतीं ? हम आज भी जंगलों में जानवरों की तरह भटकते होते ! इन अतिरिक्त सुविधाओं के लिए सभी ने जाने-अनजाने हाथ बँटाया है, यह उन्होंने पैदा की हैं। जो उनके लिए तरस रहे हैं। व्यक्ति इत्र छिड़ककर फूल सूँघता हुआ इन फटेहालों के बीच से निरपेक्ष होकर गुज़र सकता है, आदमी नहीं। व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, आदमी स्वतन्त्रता चाहता है। सुरक्षा और स्वतन्त्रता में बड़ा अन्तर है। स्वतन्त्रता एक का नहीं, सबका अधिकार है !’’
डैडी ऊबने लगे थे। ममी ने चाय के लिए आवाज लगाई। मैं तो सचमुच खो गई थी। मन होता था, सिल्क के कपड़े उतार फेंकूँ। उस दिन पहली बार मुझे इस खोखली जिन्दगी के अतिशय बनाव-श्रृंगार, तौर-तरीकों, हाव-भावों में अरुचि हुई थी। जीवन की अर्थहीनता और व्यर्थ नाटकीयता तथा बनावट से असंतोष हुआ था। क्या मैं इनसे बड़ी बातों के लिए नहीं जी सकती ? दिन-भर केवल यह देह क्यों सजाती हूँ ? शीशे में घण्टों परछाईं से बातें क्यों करती हूँ ? न जाने कैसी श्रद्धा उपजी थी उस दिन ! पर डैडी और ममी के चेहरे उतरे हुए थे, जैसे उनके जीवन-भर के श्रम को किसी ने व्यर्थ कर दिया हो।
चाय आयी और हम पीने बैठ गये। इतने में भाई साहब और जितेन आ गये। वातावरण हलका हुआ। जितेन ने मुसकराते हुए कहा, ‘‘मैं बता सकता हूँ कि इस वक़्त कौन-सा सेण्ट महक रहा है !’’ कहते हुए उसने उड़ती नज़र सब पर डालकर मेरी ओर देखा और खिलखिलाकर हँसते हुए बोला, ‘‘चम्पा !’’
ममी ने चाय पीते हुए प्रशंसा से भरकर कहा, ‘‘जितेन बड़ा तेज है।’’
सबकी नजरों में प्रशंसा झाँकने लगी।
जितेन ने डैडी के पैरों की ओर देखते हुए कहा, ‘‘अंकिल, अब आप यह पतली टो का जूता पहनना छोड़ दीजिए !’’
‘‘मैंने ब्राड-कप-शेप बनवाया है !’’—भाई साहब ने कहा।
बेदम मछलियाँ फिर पानी में पहुँच गयीं।...जू में नया चीता आया है।...हिन्दी पिक्चर्स बेकार होती हैं। ....इस बार भी डर्बी की प्राइज किसी अमेरिकी व्यापारी को मिली है।...
दिवाकर फिर संकुचित होने लगा। कैसे बैठे हो, दिवाकर ! कोई पूछ लेता, तो शर्तिया उठकर भाग जाता। जितेन की बातों से मेरा मन ऊबने लगा। मुझे लगा कि दिवाकर मेरा उठ जाना पसन्द करेगा। मैं उठ गयी।
उस दिन से अजीब कशमकश रहती। मेरा मन होता कि सबको छोड़कर दिवाकर का हाथ पकड़ लूँ और कहूँ, चाहे जहाँ ले चलो। मैं स्वतन्त्र हूँ। तुम्हें अपना मान चुकी हूँ। तुम्हारी आग मुझे आकर्षित करती है। सचमुच जीवन में सुरक्षित क्या है ? तुम अपनी मुक्ति में मुझे भी बाँध लो। मेरे जीवन का छूटा हुआ सत्य मुझे दे दो !..
एक रात सपना देखा। दिवाकर के साथ न जाने कहाँ-कहाँ घूम रही हूँ। वह जहाँ भी जाता है, लोग प्यार से उसे घेर लेते हैं। वापसी पर वह बहुत थक गया है। पर रात गए तक वह मेज़ पर झुका घण्टों बैठ लिखता रहा। मैंने पीछे से जाकर उसके छितराए हुए बालों को चूम लिया। फिर उसकी बाँहों के घेरे। नहीं....नहीं...इसे पूरा कर लो, दिवाकर...और देर बाद थक कर वह मेरी गोद में पड़ा निश्शंक, निर्द्वन्द्व सो रहा है। आँखें खुलीं तो कुछ भी नहीं था। मैं निपट अकेली थी।
न जाने वह क्या-क्या बताया करता था। एक दिन बोला था, ‘‘अपनी ज़िंदगी जियो मीना ! तुम्हारा सौंदर्य के प्रति अनुराग मुझे अच्छा लगता है, जहाँ तक वह तुम्हारा है। लेकिन जब तुम लोग नक़ल करते हो तो बौने लगते हो। तुम जीवनियाँ पढ़ती हो। वे इसलिए आकर्षिक करती हैं कि वे उन लोगों की अपनी हैं। राहुल की जीवनी पढ़कर कितनों ने विद्रोह नहीं किया होगा ! भागे होंगे। लेकिन किसी का नाम सुनाई पड़ता है ! कोई कुछ कर पाया ? अपनी मौलिकता सबसे बड़ी निधि है। उन जीवनियों की सतत प्यास को पहचानों ! यह तुम्हारा फूलों का प्यार, यह हर शाम की एक-सी मुस्कान, पपी को गोद में लेकर सहलाना और रटे हुए वाक्यों की बौछार, यह एकसरता धीरे-धीरे तुम्हें निर्जीव बना देगी...’’
मैं बहुत सोचती उन बातों पर, और मुझे लगता कि मैं दिवाकर को बेहद चाहने लगी हूँ। लेकिन उस दिन के बाद में उसकी आलोचना होने लगी। कभी दिवाकर का जिक्र आता, तो ममी कहतीं, ‘‘दिवाकर जान-बूझकर अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है। उसका यह ऊट-पटाँग सोचना और लिखना-लिखाना किस काम आयेंगे ! कल ठोकरें खायेगा, तब दिमाग़ रास्ते पर आ जायेगा।’’
मैं सुनती तो ठिठक जाती। पहले ममी की जबान उसकी तारीफ़ करते नहीं थकती थी। आखिर उस दिन उसने ऐसा क्या-कुछ कह दिया, जो सबका दिमाग़ पलट गया। उसकी बुराई होती तो मुझे चुभती।
उस दिन के बाद दिवाकर का स्वागत रूखा होने लगा। डैडी धीरे से मुसकराकर उठ जाते। ममी इधर-उधर की बातें करके जैसे टालने लगीं। उसके जाते ही हजारों बातें शुरू हो जातीं, इन लेखकों-सुधारकों का कोई ठिकाना है ? न जाने क्यों, डैडी और ममी दिवाकर को लेखक पुकारते थे और सुधारकों से उसकी तुलना करते थे !.....ये लोग तो मिराकी होते हैं। ग़रीबों की हिमायत करते हैं और उन्हीं का ख़ून चूसते हैं ! अच्छा-ख़ासा तेज़ लड़का था। किसी तरफ़ लगता तो चमक जाता। नेता हो गया है। ऊटपटाँग कपड़े पहनता है....’
धीरे-धीरे उसका आना कम होता गया। जितेन अब भी आता था। दिवाकर की ख़बर मिलनी भी कम हो गयी। मुझे उसकी याद आती थी। उसके साथ बिताये क्षण याद आते थे। पर जो करना चाहती थी, वह नहीं हो पाता था। कभी वह आता तो सबकी नज़रें मेरी तरफ़ रहतीं। उसके साथ उठने-बैठने, घूमने-घामने पर अदृश्य पाबंदी-सी लगी दिखाई देती। वह भी न जाने कैसा हो गया था। जिन बातों से डैडी और ममी को चिढ़ होती थी, वही अदबदाकर करता। जान-बूझकर खद्दर पहन आता। कलीदार कुरता पहनकर अजीब तरह से बातें करता। मैं उसके लिखे पत्रों के खोलकर पुरानी बातें याद करती। समय-समय पर उसकी भाव-भंगिमाएँ याद करती। पर एक दिन ममी ने बहुत अपनेपन से कहा, ‘‘मीनू, तू नाहक उलझी रहती है। ज़िन्दगी को इस तरह नहीं लेते। कोई अपने को योग्य साबित न कर सके, इसमें उसकी ग़लती है, तेरी नहीं।’’
और एक दिन दिवाकर मुझे अकस्मात् अशोक रोड पर मिल गया। कहने लगा, कहीं बाहर जा रहा है। मैं जाने क्यों उससे अधिक बात नहीं कर पायी। घर पहुँचने की जल्दी थी। घर आते ही जितेन इन्तज़ार करते मिला। ममी और डैडी ड्राइंगरूम में ही बैठे थे। मुझे देखते ही जितेन बोला, ‘‘चलिए आंटी, मीना भी आ गयी, अब प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता।’’ और उस रात हम सिनेमा चले गये। जितेन मुझे चारों ओर से ऐसे घेरे रहा, जैसे मैं उसकी हूँ। बड़ी अनूठी अनुभूति हुई उस रात। जितेन रास्ते-भर पिक्चर की तारीफ़ करता रहा, विशेषकर इटैलियन नर्तकी की। उसकी चेष्टाएँ अनदेखे ही बढ़ती गयीं। ममी की ओर संकोच से मैंने देखा। वह असंतुष्ट थीं। उनके व्यवहार में छूट और इस ओर से लापरवाही थी।
दिन बीतते रहे। दिवाकर कहीं-न-कहीं मिलता रहा। कभी-कभी मुझे यह भी लगता कि उसका यह मिलना आकस्मिक नहीं होता। एक रोज़ मैं ऊपर वाले कमरे में थी। सड़क पर दिवाकर का भ्रम हुआ, कुछ देर बाद फिर भ्रम हुआ, शायद वह वापस जा रहा था। मैं उतरकर नीचे लॉन में आ गयी। कुछ देर बाद वह फिर गुज़रा। उसने उड़ती हुई निगाह मेरी ओर डाली। मुझे देखा और निकल गया। मैं इन्तज़ार करती रही कि वह अब वापस आये तो रोक लूँगी, पर वह नहीं आया।
और इसके बाद वह दिन...
शाम थी। सभी लोग बैठे गपशप कर रहे थे। जितेन के क़हक़हों से कमरा गूँज रहा था। वह कह रहा था, ‘‘हिन्दुस्तान की इमारतों का क्या देखना ? इमारतें देखना है तो अमेरिका की देखिए। आरामदेह और खूबसूरत ! सादगी और खूबसूरती में अमेरिका मॉडल का जोड़ नहीं ! मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि जिसने अमेरिका नहीं देखा, वह इंजीनियर हो ही नहीं सकता !’’
‘‘इसमें क्या शक !’’ भाई साहब बोले।
‘‘ग़नीमत है कि शर्माजी यहाँ नहीं हैं, नहीं तो अमेरिका की इमारतों का सम्बन्ध वेदों से जुड़ गया होता !’’ जितेन ने कहा और हम सभी हँस पड़े। मैं क्यों हँसी, शायद जितेन के कारण।
तभी भाई साहब ने उसी मज़ाक़ के दौरान कहा, ‘‘श्री दिवाकर जी हिन्दी-प्रचारक होकर आसाम चले गये हैं।’’
श्री और जी सुनकर जितेन हँस पड़ा। बोला, ‘‘आसाम के जंगलों में ! आखिर हिन्दी संस्किरित की बेटी है !’’
सुनकर डैडी मुसकरा दिये।
मुझे एकाएक कुछ बुरा-सा लगा, यह सोचकर कि वह कितनी दूर चला गया। अकेला गया होगा। और उसके बाद दिवाकर का कोई समाचार नहीं मिला।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book