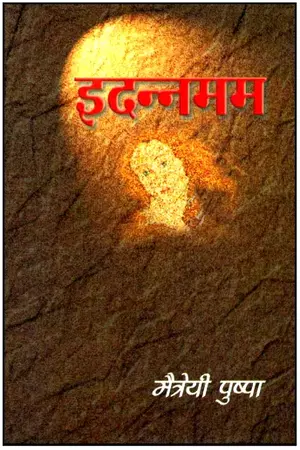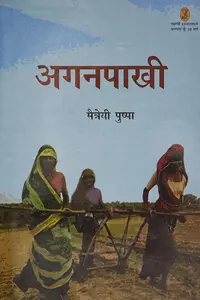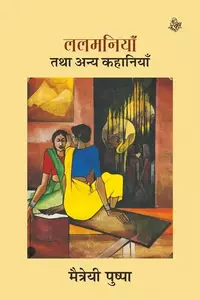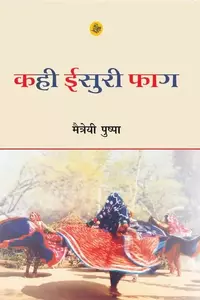|
नारी विमर्श >> इदन्नमम इदन्नमममैत्रेयी पुष्पा
|
445 पाठक हैं |
|||||||
समकालीन कथा-लेखन में सक्रिय एक सशक्त हस्ताक्षर मैत्रेयी पुष्पा की कलम से निकली औपन्यासिक कृति इदन्नमम
Idannam
प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश
समकालीन कथा-लेखन में सक्रिय एक सशक्त हस्ताक्षर मैत्रेयी पुष्पा की कलम से निकली औपन्यासिक कृति इदन्नमम में बुनी गई है तीन पीढ़ियों की बेहद और संवेदनाशील कहानी जो बऊ (दादी), प्रेम (माँ) और मंदा (उपन्यास की नायिका)-तीनों को समानांतर रखने के साथ-साथ, एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा भी करती है। विरोधाभास की इस प्रतीति को लेखिका ने सक्षमता, सूक्ष्मता और परामर्श भाषाजाल से बुना है, जो अत्यंत पठनीय है और अपने स्वर में मौलिक भी।
इदन्नमम के आँचल में छिपा है विंध्य का अंचल। विंध्य की पहाड़ियों से घिरे वर्णित गाँव श्यामली और सोनपुरा के जन-जीवन की जीवंत धड़कनों को यह उपन्यास साँस-दर-साँस कहता है और पाठक को लगता है मानो वह पूरे आंचल में कदम-कदम चल रहा है। इन गाँवों में अंचल में धूल है, नदी है, पर्व हैं, गीत हैं, आहें-कराहें हैं, सत-असत है और रुढ़ियों और परंपराओं की भरी-पूरी दुनिया। उपन्यास के अंचल की इस दुनिया में आकांक्षा है, ईर्ष्या है और उन पर झपटते भेड़िए हैं उन्हें त्यागते साधु हैं तथा हैं हाड़-मांस के सौ फीसदी पात्र! शोषित होने से इंकार करते ये पात्र इस उपन्यास की अतिरिक्त विशेषता हैं।
वरिष्ठ कथाकार राजन्द्र यादव के शब्दों में कहें तो इदन्नमम में ‘‘मिट्टी-पत्थर के ढोकों या उलझी डालियों और खुरदुरी छाल के आसपास की सावधान छँटाई करके आकृतियाँ उकेर लेने की अद्भुत निगाह है...लगभग ‘रेणु’ की याद दिलाती हुई।’’
वास्तव में घनीभूत संवेदना और भावनात्मक लगाव से लिखी गई इदन्नमम की कहानी समकालीन हिंदी उपन्यास जगत में एक घटना है, जिसका स्वागत किया जाना अभीष्ट है।
इदन्नमम के आँचल में छिपा है विंध्य का अंचल। विंध्य की पहाड़ियों से घिरे वर्णित गाँव श्यामली और सोनपुरा के जन-जीवन की जीवंत धड़कनों को यह उपन्यास साँस-दर-साँस कहता है और पाठक को लगता है मानो वह पूरे आंचल में कदम-कदम चल रहा है। इन गाँवों में अंचल में धूल है, नदी है, पर्व हैं, गीत हैं, आहें-कराहें हैं, सत-असत है और रुढ़ियों और परंपराओं की भरी-पूरी दुनिया। उपन्यास के अंचल की इस दुनिया में आकांक्षा है, ईर्ष्या है और उन पर झपटते भेड़िए हैं उन्हें त्यागते साधु हैं तथा हैं हाड़-मांस के सौ फीसदी पात्र! शोषित होने से इंकार करते ये पात्र इस उपन्यास की अतिरिक्त विशेषता हैं।
वरिष्ठ कथाकार राजन्द्र यादव के शब्दों में कहें तो इदन्नमम में ‘‘मिट्टी-पत्थर के ढोकों या उलझी डालियों और खुरदुरी छाल के आसपास की सावधान छँटाई करके आकृतियाँ उकेर लेने की अद्भुत निगाह है...लगभग ‘रेणु’ की याद दिलाती हुई।’’
वास्तव में घनीभूत संवेदना और भावनात्मक लगाव से लिखी गई इदन्नमम की कहानी समकालीन हिंदी उपन्यास जगत में एक घटना है, जिसका स्वागत किया जाना अभीष्ट है।
अप्प दीपो भव
महानगरीय मध्यवर्ग की संघर्ष करती और पाँवों के नीचे जमीन की तलाश करती कथा-नारियों के बीच गाँव की मंदा एक अजीब निरीह, निष्कवच, निश्छल संकल्प-दृढ़ नारी का व्यक्तित्व लेकर उभरती है—बाढ़ के बीच धीरे-धीरे उगते टीले या द्वीपों की तरह, मगर वह द्वीप नहीं है, उसके साथ है एक भरी-पूरी दुनिया-रूढ़ियों, परंपराओं, अभ्यासों, आकांक्षाओं-ईर्ष्याओं से भरी—एक-दूसरे के अधिकार झपटते, कुचलते, चूसते और न्याय की रक्षा करते लोगों की जिंदगी। मंदा को इन्हीं के बीच रहना और रास्ता निकालना है। उसकी लड़ाई दुहरी है, होने की और वंचितों के अधिकारों की....
बऊ (दादी), प्रेम (माँ) और मंदा...तीन पीढ़ियों की यह बेहद सहज कहानी तीनों को समानान्तर भी रखती है और एक-दूसरे के विरुद्ध भी। बिना किसी बड़बोले वक्तव्य के मैत्रेयी ने गहमागहमी से भरपूर इस कहानी को जिस आयासहीन ठंग से कहा है, उसमें नारी-सुलभ चित्रात्मकता भी है और मुहावरेदार आत्मीयता भी। हिन्दी-कथा-रचनाओं की सुसंस्कृत सटीक और बेरंगी भाषा के बीच गाँव की इस कहानी को मैत्रेयी ने लोक-कथाओं के स्वाभाविक ढंग से लिख दिया है, मानो मंदा और उसके आसपास के लोग खुद अपनी बात कह रहे हों—अपनी भाषा और अपने लहजे में, बुंदेलखंडी लयात्मकता के साथ...अपने आसपास घरघराते क्रेशरों और ट्रैक्टरों के बीच।
मिट्टी-पत्थर के ढोकों या उलझी डालियों और खुरदरी छाल के आसपास की सावधान छँटाई करके सजीव आकृतियाँ उकेर लेने की अद्भुत निगाह है मैत्रेयी के पास—लगभग ‘रेणु’ की याद दिलाती हुई। गहरी संवेदना और भावनात्मक लगाव से लिखी गई यह कहानी बदलते, उभरते, ‘अंचल’ की यातनाओं, हार-जीतों की एक निर्व्याज गवाही है....पठनीय और रोचक।
कामना करता हूँ कि ‘विशिष्ट और महत्वपूर्ण’ होने का बोध जगाने से पहले ही मैत्रेयी कुछ और इतना ही सहज लिख डालें—सेमिनारों-गोष्ठियों में जगमगाते शहरी रचनाकार होने के प्रलोभनों से अपने को बचाए रखते हुए....
बऊ (दादी), प्रेम (माँ) और मंदा...तीन पीढ़ियों की यह बेहद सहज कहानी तीनों को समानान्तर भी रखती है और एक-दूसरे के विरुद्ध भी। बिना किसी बड़बोले वक्तव्य के मैत्रेयी ने गहमागहमी से भरपूर इस कहानी को जिस आयासहीन ठंग से कहा है, उसमें नारी-सुलभ चित्रात्मकता भी है और मुहावरेदार आत्मीयता भी। हिन्दी-कथा-रचनाओं की सुसंस्कृत सटीक और बेरंगी भाषा के बीच गाँव की इस कहानी को मैत्रेयी ने लोक-कथाओं के स्वाभाविक ढंग से लिख दिया है, मानो मंदा और उसके आसपास के लोग खुद अपनी बात कह रहे हों—अपनी भाषा और अपने लहजे में, बुंदेलखंडी लयात्मकता के साथ...अपने आसपास घरघराते क्रेशरों और ट्रैक्टरों के बीच।
मिट्टी-पत्थर के ढोकों या उलझी डालियों और खुरदरी छाल के आसपास की सावधान छँटाई करके सजीव आकृतियाँ उकेर लेने की अद्भुत निगाह है मैत्रेयी के पास—लगभग ‘रेणु’ की याद दिलाती हुई। गहरी संवेदना और भावनात्मक लगाव से लिखी गई यह कहानी बदलते, उभरते, ‘अंचल’ की यातनाओं, हार-जीतों की एक निर्व्याज गवाही है....पठनीय और रोचक।
कामना करता हूँ कि ‘विशिष्ट और महत्वपूर्ण’ होने का बोध जगाने से पहले ही मैत्रेयी कुछ और इतना ही सहज लिख डालें—सेमिनारों-गोष्ठियों में जगमगाते शहरी रचनाकार होने के प्रलोभनों से अपने को बचाए रखते हुए....
इदन्नमम
एक
बेर की कँटीली झाड़ियों और गूलर के पेड़ों से आच्छादित गैल से निकलकर बैलगाड़ी सड़क पर आ लगी।
सड़क-सड़क चलते ही लिपी दीवारों वाले घरौंदों की खपरैलें तथा बीच गाँव में बने पक्के अटाओं की झिलमिलाती सफेदी दिखाई पड़ने लगी।
छतों पर झुके पेड़ रूखों की हरियाली को देखकर बैलों को हाँकते हुए पक आयी उम्र के गनपत बोले, ‘‘लो बऊ, आ गया श्यामली गाँव।’’
सुनते ही बऊ के गेहुआँ रंग के बूढ़े चेहरे पर हड़बड़ाहट छा गयी। ऐनक नाक के ऊपर से नीचे सरक आयी, नाक में पहनी सतबुँदिया लौंग के ऊपर। उन्होंने होंठ सिकोड़ लिए, जिसके कारण नाक अधिक नुकीली-सी दिखने लगी।
चश्मा साधकर उन्होंने निगाह तेरह वर्षीय मन्दाकिनी पर डाली जो गाड़ी में बिछे खेस पर बेसुध सो रही थी और फ्रॉक सिकुड़ जाने से जिसकी जाँघें खुल आयी थीं।
‘‘फिराक नहीं बदली मोंड़ी ने ! बिराने गाँव में ऐसे ही...उघारे गोड़ ! सिलवार-कुरता पहर लेती तो ठीक रहता।’’
‘‘बखत ही नहीं मिला होगा। नहीं तो मन्दा फिराक पहरकर आने वाली नहीं थी। हमारे दुख के कारण बोल नहीं पायी स्यात।’’
‘‘आग लगे मोरी बूड़ी छाती कों ! पछरा पर गये बुद्धि पर ! ख्याल ही नहीं किया कुछ। ऐसी सिर्रिन बाबरी हो गयी।’’
‘‘लो जिन्दगी-भर गिरिस्ती अकेलें खेंची। महेन्दर को पाल-पोसकर बड़ा किया अकेली ने ही, और आज ऐसी निबल हो उठी। कतई हिम्मत छोड़ बैठी !’’ बऊ एकालाप में डूबी थीं।
‘‘लै आज तोय कौल है महेन्दर मताई ! पराये गाँव का सीवान नाँखने जा रही है, जो आँख से कबहुँ अँसुआ डारै।’’ बऊ ने सौगन्ध धरी अपने ही ऊपर। अपनी छाती पर हथेली जमा ली, जैसे प्रण ले रही हों। साथ ही मोह के गीलेपन से प्रयत्नपूर्वक। अपने चित्त को झटके से उखाड़ लिया। कटी जड़ों में टीसते दर्द को पीती हुई वे आगे बढ़ी चली जा रही हैं।
ऊँचे मन्दिर के पास से बैलगाड़ी ने सड़क छोड़कर गाँव के भीतर को मोड़ लिया। चौड़ी गली से गुजरती, नालियों को नाँखती उनकी गाड़ी पंचमसिंह के द्वार से जा लगी।
कुछ देर गनपत यों ही बैलों की रास थामे खड़े रहे।
न उनको ही कुछ सूझा, न बऊ को।
बऊ का मन अजीब-सी दुविधा में फँसा है कि यहाँ आकर आज उन्हें चैन की साँस लेनी चाहिए या इस अपरिचित गाँव में अपने प्रति और भी सचेत, सतर्क हो जाना चाहिए।
जिस बोध से चली थीं, वही डगमगाने लगा।
उन्होंने अपनी दुश्चिंता को काटने का प्रयास किया—पंचमसिंह ने जान लिया होगा कि अब हमारा धनी-धोरी गाँव-आनगाँव में कोई है नहीं। तभी तो बुला लिया अपने यहाँ। तभी जिम्मेदारी लेने का वचन दिया है। महीन धागे-सी रिश्तेदारी कह लो या उनका बड़ा कलेजा, नहीं तो कौन पड़ता है किसी की आपदा में !
वे अपने-आप को समेटती-सहेजती बोलीं, ‘‘गनपत, तुम ऐसे ही काहे ठाड़े रह गये ? गाड़ी खोलो।’’
गनपत ने गर्दन मोड़कर देखा, ‘‘लो तुम उतरो तो सही। गाड़ी का मुख नीचे को दबाना पड़ेगा।’’ कहकर गनपत अपने नाटे कद के कारण उछलते हुए उतर पड़े। सिर के काले-सफेद बालों में चमकता पसीना पोंछने लगे और फिर अँगोछा गर्दन के आसपास लपेट लिया।
बऊ ने चश्मे की कमानी नाक पर ठीक से बिठाई। धोती के पल्ले को सही किया, चेहरे पर माथे तक का घूँघट सरकाकर मन्दाकिनी को झकझोरकर जगाने लगीं।
‘‘मन्दा ! उठ बिटिया ! उठ तो !’’
वह हड़बड़ाती हुई उठ बैठी।
साँवली रंगत के स्निग्ध गालों पर मोटे खेस की बुनावट के निशान स्पष्ट ऊभर आये हैं। कड़क धूप से देह तप गयी है। गर्दन पर बिखरे बाल पसीने से तर हैं। मुख तमतमाकर लाल हो आया...कैसा भेस हो गया है मोंड़ी का ! बऊ भीतर पिघल उठीं।
सिर पर हाथ फेरती हुई बोलीं, ‘‘मुँह पोंछ डालो बेटा।’’
उसकी अधमुँदी पलकों के बीच पुतलियाँ चैतन्य नहीं हो पा रहीं। नींद का गहरा प्रभाव है। कुछ देर ऊँघती हुई बैठी रही। सिर दोनों बाँहों और घुटनों पर टिका लिया।
बऊ ने फिर हटोका, ‘‘उठो बिन्नू।’’
मन्दाकिनी पलकें मूँदें हुए ही बोली, ‘‘बऊ, आ गया श्यामली ?’’
‘‘और क्या ! आ नहीं गया !’’
‘‘उतरें बऊ ?’’ कहते हुए उसने अपनी सीपी-सी आँखें खोल दीं।
‘‘लो, इतेक देर से हम और क्या कह रहे हैं। पर पहलें अपनी फिराक-ठीक-ठाक कर लो।’’
बऊ ने बच्ची का कंधा थपथपा दिया।
वह खड़ी हो गयी। अपनी हरे रंग की फ्रॉक झाड़-झूड़कर नीचे को सरका ली। खेस के नीचे से नीली पट्टी वाली हवाई चप्पल निकालीं, पहनकर खड़ी-खड़ी, हाथ फेर-फेरकर अपने बालों को ठीक करने लगी। ज्यों कंघी से ओंछकर एक-से कर रही हो।
उधर के पहिये पर पाँव टिकाकर बऊ उतरीं और इधर की ओर मन्दाकिनी। बऊ कुछ देर तक लम्बी कद-काठी के चलते अकड़ी हुई कमर को सीधी करने के यत्न में खड़ी रहीं। फिर पाँवों में पहने चाँदी के लच्छे, जो आपस में उलझ-से गये थे, ठीक से बिठाये।
गनपत ने दोनों बैलों के रस्से नीम के तने से बाँध दिये। पिछौरा बँधा चारा उनके सामने खोलकर रख दिया और गाड़ी को जुआ झुकाकर एक ओर टिका दिया। अपना अँगोछा कंधो पर डालकर वे हाथ से पसीना पोंछते हुए बैलों के पास ही जमीन पर जा बैठे।
उनके बैठते ही बऊ कड़क आवाज में बोलीं, ‘‘द्वार खटकाओ गनपत।’’
अपनी आवाज में समायी बुलन्दी पर उन्हें स्वयं अचरज हुआ। लगा कि वे तो आज उसी लय में बोल रही हैं, जैसे अपनी बाखर में मईदारों को हुक्म सुनाया करती थीं और जिसे कुछ समय से भूलती जा रही हैं।
मन्दाकिनी ने निगाह घुमा-घुमाकर चारों ओर देखा। वीरानी को देखकर पूछने लगी, ‘‘यहाँ तो कोई नहीं है बऊ ! तुम तो कहती थीं, पंचमसिंह दादा के घर में बहुत-बहुत सारे लोग हैं !’’
बऊ ने अपनी धोती का पल्ला अच्छी तरह से कमर में खोंसा, नरम आवाज में बताने लगीं, ‘‘खेत कटनईं के दिन हैं बेटा, सब जने खेतों, खलिहानों में होंगे। घर की जनी-मानसें भी रोटी-पानी लैकें वहीं गयी होंगी।’’
बच्ची दो क्षण कुछ सोचती रही, सहसा चुप्पी तोड़ते हुए बोली, ‘‘हमारा खेत तुमने क्यों नहीं कटवाया बऊ ? कौन कटबायेगा। ?’’
बऊ के भीतर पैनी धार उतर गयी, क्या उत्तर दें इस प्रश्न का ? दो पल निरीह-सी देखती रहीं, फिर गहरा श्वास भरती हुई कहने लगीं, ‘‘भगवान कटबायेगा अब। अब उसी पनमेसुर के ऊपर छोड़ा है।’’
दादी का सूक्त वाक्य सम्भवतः बच्ची की समझ में नहीं आया। वह उन्हें उसी तरह प्रश्नवाचक नजरों से देखती रही।
कलईपुती दीवारें। किशमिशी रंग की चिकनी और पीतल की पीली कील-ठुकी किवाड़ें। मन्दाकिनी छू-छूकर देखने लगी।
घने नीम के हरियल वृक्ष की ओर देखती हुई बोली, ‘‘बऊ, अपने द्वार जैसा ही लग रहा है न इस घर का द्वार ?’’
बऊ ने ‘हाँ’ कहते हुए सिर हिलाया और महीन-सी हँसी हँस दी—‘‘सारे जमींदारों की हवेलियों की गढ़त एक-सी होती है स्यात।’’
दुबारा-तिबारा किवाड़ें भड़भड़ाने पर भारी चरमराहट के साथ द्वार खुला। किवाड़ों के बीच एक महिला खड़ी दिखाई दीं।
वे साँवली रंगत और मझोले कद की हैं। बीच की उम्र है। तरुणी न वृद्धा। हरी फूलदार किनारी वाली गुलाबी रंग की धोती पहने हुए। घूँघट माथे तक है। गले में सोने की हँसुली चमक रही है। बऊ ने उन्हीं पल-छिनों में सारा कुछ देख लिया।
‘‘सीताराम !’’ गनपत ने उनसे झुककर अभिवादन किया।
‘‘खुसी रहो, कहाँ सेऽऽऽ ?’’ उनका एक हाथ किवाड़ पर टिका था।
‘‘सोनपुरा से। महेन्दरसिंह की मतारी हैं हमारे संग। उनकी बिटिया मन्दा भी।’’ गनपत ने तर्जनी से इंगित कर दिया।
सुनकर एक पल को महिला का मुख विवर्ण हो आया।
कुछ देर अवाक् खड़ी रहीं।
जब सँभलीं तो पूछा, ‘‘जो मर गये थे, वे ही महेन्दरसिंह ? वे, जिनकी जनी...’’
गनपत ने स्वीकृति में सिर हिलाया।
‘‘दइया !’’ उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा।
बाहर की ओर गौर किया तो देखा कि कुछ दूरी पर एक वृद्धा, लगभग बारह-तेरह वर्ष की बच्ची को अपने से सटाये खड़ी हुई हैं। उनका हाथ बच्ची के सिर पर है और स्वयं कुछ। झुकी हुई-सी।
अभिवादन करने के लिए वे आगे बढ़ीं और बऊ के चरणों में झुक गयीं।
अधबीच ही रोक लिया बऊ ने। कंधे पकड़कर ऊपर उठा लिया।
‘‘पाँव जिन छुओ। रिस्ते में तुम हमारी भतीजी लगती हो। पंचमसिंह के घर से ही हो न ? देवगढ़वारी ?’’
‘‘हओ।’’
‘‘हम तुम्हारे पिता की फुआ की बेटी हैं, और यह हमारी पोती।’’ कहकर बऊ ने मन्दाकिनी को हाथ पकड़कर आगे कर लिया।
‘‘भीतर आ जाओ।’’ वे दोनों आगे हो लीं।
पौर में खटिया नवाती हुई सोच में बिंध गयीं, दादा ने तो इनकी आवाजाई को लेकर कुछ कहा नहीं। क्या करें ? क्या दुआरे से ही वापिस कर दें, या अपरिचित बनी रहकर किवाड़ें मूँद लें ? अब जो भी हो, द्वार आयी पाहुनी हैं। स्यात रहना भी हो इन्हें यहाँ, कि जाना हो....
खटिया बिछी तो बऊ बैठ गयीं। मन उठंग है। अधबीच लटका हुआ। मन्दाकिनी सहमी-सी एक ओर खड़ी अपनी लाल रिबन बँधी मोटी चोटी से खेल रही है।
वे बच्ची के पास पहुँच गयीं, ‘‘सरमा रही हो तुम ? हम कक्को हैं। घर-गाँव के सब लरका-बिटिया हमें ‘कक्को’ कहकर बुलाते हैं, तुम भी कक्को कहो।’’ उन्हें मन्दाकिनी को देखकर ममता उमड़ आयी। उसकी पीठ को सहारा देती हुई वे खटिया तक ले आयीं और अपने से सटाकर बिठा लिया।
वे देखती रहीं, बच्ची की आँखें कजरारी, घनी लम्बी बरौनियों वाली हैं, जिन्हें वह पटर-पटर झपका रही है। खाने वाला मुँह छोटा है, ऊपर का होंठ धनुष की तरह कटावदार और ललामी लिए हुए। मुख पर झलकती उम्र के मुकाबले कद लम्बा है। टेढ़ी माँग निकालकर बाल सँवारे हैं और एक लट अंडे की सी बनगत वाले चेहरे पर बार-बार झूल जाती है, जिसको सिर झटककर वह पीछे कर लेती है।
‘‘बहू जा बिटिया को छोड़कें चली गयी।’’ वे बऊ से मुखातिब हुईं।
बऊ कुछ न बोलीं, जैसे चुप्पी के परदे में स्वयं को छिपा रही हों।
‘‘पानी ले आवें हम। प्यास लगी होगी।’’ कहकर वे भीतर चली गयीं।
मन्दाकिनी खटिया पर बैठी-बैठी अपने लटके हुए पावों को हिलाने लगी थी, ज्यों पंजों को झूला झुला रही हो।
बऊ ने देखते ही हटोका, ‘‘सूधें बैठ जा मन्दा ! पाँव नहीं हिलाते, दोस होता है।’’
उसने अपने पाँवों की हरकत उसी दम रोक दी और पूछने लगी, ‘‘दोस क्यों होता है बऊ ?’’
बऊ से कोई उत्तर न बन पड़ा।
कक्को ने पानी भरा लोटा बऊ को थमा दिया। बऊ ने पानी का रंग देखा और बोलीं, ‘‘जे तो सरबत है। इतेक हमसे नहीं पिबेगा। मन्दा भी इसी में पी लेगी। और जिन लाना।’’
‘‘हमारे गनपत कक्का पियेंगे लाओ हम दे आयें,’’ मन्दा ने कहा—
वे विहँस उठीं, ‘‘तुम काहे ? हम दे आते हैं।’’
कक्को खटिया के पायँते बैठ गयीं। अब क्या बातें करे ? किस छोर की गहें ? कहाँ से आरम्भ करें ? और कहाँ अन्त ? दुख-विपता की बातें चलाना क्या आसान काम है ? जबकि मालूम हो, सामने बैठा मनिख ठहरी हुई पीर में फिर बहने लगेगा।
किस हिम्मत से छेड़ें बऊ के दुख का प्रकरण...वे चुप बैठी रहीं।
बातें बऊ से भी नहीं बन पा रहीं। पराया गाँव। बिरानी माँटी। अनचीन्ही धरती और अजनबी आसमान...जिधर को दृष्टि जाती है, अलगाव-सा झरता दीखता है।
बऊ गुमसुम बैठी रहीं।
देखती रहीं, मन्दा का मुख मलिन है। बाल उलझे हुए। फ्रॉक पर जगह-जगह मटमैले धब्बे लगे हैं।
उसका ध्यान भी अपनी फ्रॉक पर है।
बऊ ने गरदन में हाथ डालकर, कान के पास मुँह ले जाकर कहने लगी, ‘‘उठो बऊ, बक्सा खोलो। हम कपड़ा बदलेंगे।’’
उन्होंने धीरे से उसका हाथ दबा दिया, ‘‘अबै नहीं। तनक गम खाओ। रुकने-बैठने का ठौर...’’
अब वे दोनों बरामदे में खेस बिछाकर बिठा दी गयीं।
‘‘बऊऽऽ !’’ मन्दाकिनी ने अपनी फ्रॉक दिखाकर फिर ध्यान दिलाया।
‘‘मन्दा, तुम भी बड़ी जिद्दिन हो। कह तो रहे हैं, अबै कहाँ से निकार दें तुम्हारे उन्ना कपड़ा ? कित्तै धर के खोलें बक्सा ?’’ बऊ खीजी-सी फुसफुसाईं।
घर की स्त्रियाँ अपने कामों से फुरसत पाकर उनके पास आ बैठीं।
बातें चल उठीं। मिल-जुलकर उसी विपत्ति की परतें उखाड़ी जाने लगीं, जिससे वे कतई बचना चाहती हैं।
‘‘लो भाग तो देखो कि इतेक मुसीबत।’’
दूसरी बोली, ‘‘भाग-कुभाग की क्या बात, इनकी बहू ने ही संग नहीं दिया, तो फिर कोई गैर कैसे समझेगा इनकी पीर ?’’
मन्दाकिनी देख रही है, इन औरतों के गोदों में बच्चे हैं। छाती से दूध चूसते हुए बच्चे। गोदी में बैठकर खुश होने वाले बच्चे। एक-दो गोद में बैठकर भी रोने वाले बच्चे, जिन्हें वे अनजाने की थपथपा देती हैं और छूटी हुई बात का छोर गहकर बऊ को फिर खींच लेती हैं चर्चा में।
‘‘जीजा के संग भग गयी।’’ एक ने कहा।
‘‘भग कहाँ गयी अपहरन हुआ है बेचारी का।’’ दूसरी ने तर्क दिया।
‘‘अई, नोंनें रहो। अपहरन काहे ! अपहरन होता तो बऊ का न हो जाता। जे भी तो भर ज्वानी में विधवा हुई थीं। जे कहो कि मस्तानी हती। ज्वानी की मारी। सो बिना खसम के रहाई नहीं आयी।’’
बऊ की भीतरी परतें छिलने लगीं। सुनते-सुनते आँखों में नमी आ गयी। मन्दाकिनी कुछ देर तक उन औरतों को घूरती रही। उसके होंठ भिंच गए, आँखें बड़ी और पनीली-सी दिखने लगीं। बऊ को अधिक उदास देखकर उनके घुटने पर अपना सिर टिका दिया।
सहसा वे सब द्रवित-सी हो गयीं, बोलीं, ‘‘देखो तो, मोंड़ी हिंरस उठी। कैसी कठकरेज मतारी हती कि छोड़ गयी पुतरिया-सी बिटिया कों ! चिरइया-परेबा तक नहीं छोड़ते अपने अंडी-बच्चा।’’
साँझ हो आयी।
आँगन में धूप सरककर दीवारों पर पहुँच गयी।
एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण मन्दाकिनी ऊबने लगी। बऊ को संकेतों से समझाने लगी कि चलो बऊ।
वे अनदेखा किये बैठी रहीं। दादा की प्रतीक्षा है उन्हें। आ जाते तो रुख का पता चलता। भले ही सहमति है, लेकिन उनका सन्देही मन कई तरह से सोचने लगता है। न जाने किस तरह से लें उनके आने को ? हँसी-खुशी में पाहुनी बनकर थोड़े ही आयी हैं, संकटों में उलझी आगन्तुका हैं। ऐसे में कौन कर सकता है स्वागत ? अपने ही किनारा कर जाते हैं दुख-तकलीफ के बखत।
फिर दादा कहीं यह न सोचने लगें कि मातौन तो आदर के भी खा गयीं। हमने झूठे को कहा और वे साँचे को चली आयी।
दिन डूबने में जो घंटा-डेढ़ घंटा बचा है, वह उन्हें बहुत लम्बा और भारी लग रहा है। काटे नहीं कट रहा।
मन्दाकिनी की दृष्टि अब कहीं और है।
स्कूल से बच्चे लौट चुके हैं। माँओं से खाने की माँग कर रहे हैं। कक्को से घी और चीनी के लिए जिद कर रहे हैं। सब्जी देखकर मुँह बिचका रहे हैं।
कुछ बस्ते रखकर पनारे पर मुँह-हाथ धोने में लगे हैं।
उसे अजनबी निगाहों से देख रहे हैं। अनचीन्हे भाव से घूर रहे हैं।
उसने अपनी फ्रॉक के घेर को घुटनों से खींच-खींचकर दोनों टाँगें ठीक प्रकार ढक लीं और खेस के ऊपर भली प्रकार बैठ गयी।
बऊ बोलीं, ‘‘तुम ज्यादा न तानना फिराक को, फट जायेगी।’’
कतार बनाकर बोरियाँ डाली गयीं। परसी हुई थालियाँ उनके आगे रखी गयीं। थालियों में आलू-बैगन का साग, दही का कटोरा, घी से चुपड़ी हुई ठंडी रोटियाँ। मिर्च और आम का अचार।
बच्चों ने मिलकर स्वर साधा :
‘‘आलू भटा की तिरकाई, नाचे मुन्ना की मताई।’’
फिर सब हँस पड़े।
मन्दाकिनी खिलखिलाती हुई पीछे तक हँसती रही।
सबका ध्यान उसकी हँसी पर ठहर गया।
वह एकदम चुप हो गयी।
कक्को ने उसे हाथ पकड़कर उठा लिया, ‘‘चलो, तुम भी खा लो।’’
अपनी पंक्ति में उसे बैठे हुए खाते देखकर लड़के विचित्र भाव से हँसने लगे। आपस में कान पर मुँह रखकर कुछ कह रहे हैं, जिसे वह सुन तो नहीं पा रही, लेकिन समझने की कोशिश कर रही है।
इस तरह का व्यवहार उसे बिलकुल अच्छा नहीं लगा। थाली लेकर जल्दी ही उठ गयी और पनारे पर रख आयी।
लौटकर बऊ के पास आ बैठी। बेचिन्हारा स्थान, अपरिचित चेहरे जैसे उसे दुखी और तंग करने पर तुले हैं। उसे सुगना की याद आने लगी। सात-आठ साल की सुगना उसके साथ ही साथ लगी रहती थी। स्कूल से लेकर तालाब-पहाड़ सब जगह संग। सुगना की चोटी से खोलकर यह लाल रिबन काकी ने चलते समय उसकी चोटी में बाँध दिया था। हड़बड़ी में कंघी-रिबन मिले ही नहीं थे उसे। बऊ ताला लगाने की जल्दी जो मचा रही थीं।
वह गाड़ी में बैठकर चली थी तो सुगना रोने लगी थी। जगेसर कक्का ने डपट दिया था काकी को कि चलो अपने घरै। आँखों में आँसू भरे सुगना कभी पिता की ओर देखती, कभी उसकी ओर।
‘‘बऊ, सुगना के पिता जी हैं, जगेसर कक्का। पिता जी हैं तो हर समय डाँटते क्यों रहते हैं ?’’
बऊ कुछ न बोलीं।
वह रिबन को ही देख रही है। सुगना का गोरा मुख याद आ रहा है कि अचानक बच्चों के झुंड में से कोई स्वर सुनाई पड़ा :
‘‘एक फूल की चार कली, रानी डोले गली-गली।’
ये क्या चिढ़ा रहे हैं उसे ? और नहीं तो क्या ? उसने मारे गुस्से के उन शैतान बालकों की ओर से पीठ कर ली। तमतमाई-सी बैठी रही।
सड़क-सड़क चलते ही लिपी दीवारों वाले घरौंदों की खपरैलें तथा बीच गाँव में बने पक्के अटाओं की झिलमिलाती सफेदी दिखाई पड़ने लगी।
छतों पर झुके पेड़ रूखों की हरियाली को देखकर बैलों को हाँकते हुए पक आयी उम्र के गनपत बोले, ‘‘लो बऊ, आ गया श्यामली गाँव।’’
सुनते ही बऊ के गेहुआँ रंग के बूढ़े चेहरे पर हड़बड़ाहट छा गयी। ऐनक नाक के ऊपर से नीचे सरक आयी, नाक में पहनी सतबुँदिया लौंग के ऊपर। उन्होंने होंठ सिकोड़ लिए, जिसके कारण नाक अधिक नुकीली-सी दिखने लगी।
चश्मा साधकर उन्होंने निगाह तेरह वर्षीय मन्दाकिनी पर डाली जो गाड़ी में बिछे खेस पर बेसुध सो रही थी और फ्रॉक सिकुड़ जाने से जिसकी जाँघें खुल आयी थीं।
‘‘फिराक नहीं बदली मोंड़ी ने ! बिराने गाँव में ऐसे ही...उघारे गोड़ ! सिलवार-कुरता पहर लेती तो ठीक रहता।’’
‘‘बखत ही नहीं मिला होगा। नहीं तो मन्दा फिराक पहरकर आने वाली नहीं थी। हमारे दुख के कारण बोल नहीं पायी स्यात।’’
‘‘आग लगे मोरी बूड़ी छाती कों ! पछरा पर गये बुद्धि पर ! ख्याल ही नहीं किया कुछ। ऐसी सिर्रिन बाबरी हो गयी।’’
‘‘लो जिन्दगी-भर गिरिस्ती अकेलें खेंची। महेन्दर को पाल-पोसकर बड़ा किया अकेली ने ही, और आज ऐसी निबल हो उठी। कतई हिम्मत छोड़ बैठी !’’ बऊ एकालाप में डूबी थीं।
‘‘लै आज तोय कौल है महेन्दर मताई ! पराये गाँव का सीवान नाँखने जा रही है, जो आँख से कबहुँ अँसुआ डारै।’’ बऊ ने सौगन्ध धरी अपने ही ऊपर। अपनी छाती पर हथेली जमा ली, जैसे प्रण ले रही हों। साथ ही मोह के गीलेपन से प्रयत्नपूर्वक। अपने चित्त को झटके से उखाड़ लिया। कटी जड़ों में टीसते दर्द को पीती हुई वे आगे बढ़ी चली जा रही हैं।
ऊँचे मन्दिर के पास से बैलगाड़ी ने सड़क छोड़कर गाँव के भीतर को मोड़ लिया। चौड़ी गली से गुजरती, नालियों को नाँखती उनकी गाड़ी पंचमसिंह के द्वार से जा लगी।
कुछ देर गनपत यों ही बैलों की रास थामे खड़े रहे।
न उनको ही कुछ सूझा, न बऊ को।
बऊ का मन अजीब-सी दुविधा में फँसा है कि यहाँ आकर आज उन्हें चैन की साँस लेनी चाहिए या इस अपरिचित गाँव में अपने प्रति और भी सचेत, सतर्क हो जाना चाहिए।
जिस बोध से चली थीं, वही डगमगाने लगा।
उन्होंने अपनी दुश्चिंता को काटने का प्रयास किया—पंचमसिंह ने जान लिया होगा कि अब हमारा धनी-धोरी गाँव-आनगाँव में कोई है नहीं। तभी तो बुला लिया अपने यहाँ। तभी जिम्मेदारी लेने का वचन दिया है। महीन धागे-सी रिश्तेदारी कह लो या उनका बड़ा कलेजा, नहीं तो कौन पड़ता है किसी की आपदा में !
वे अपने-आप को समेटती-सहेजती बोलीं, ‘‘गनपत, तुम ऐसे ही काहे ठाड़े रह गये ? गाड़ी खोलो।’’
गनपत ने गर्दन मोड़कर देखा, ‘‘लो तुम उतरो तो सही। गाड़ी का मुख नीचे को दबाना पड़ेगा।’’ कहकर गनपत अपने नाटे कद के कारण उछलते हुए उतर पड़े। सिर के काले-सफेद बालों में चमकता पसीना पोंछने लगे और फिर अँगोछा गर्दन के आसपास लपेट लिया।
बऊ ने चश्मे की कमानी नाक पर ठीक से बिठाई। धोती के पल्ले को सही किया, चेहरे पर माथे तक का घूँघट सरकाकर मन्दाकिनी को झकझोरकर जगाने लगीं।
‘‘मन्दा ! उठ बिटिया ! उठ तो !’’
वह हड़बड़ाती हुई उठ बैठी।
साँवली रंगत के स्निग्ध गालों पर मोटे खेस की बुनावट के निशान स्पष्ट ऊभर आये हैं। कड़क धूप से देह तप गयी है। गर्दन पर बिखरे बाल पसीने से तर हैं। मुख तमतमाकर लाल हो आया...कैसा भेस हो गया है मोंड़ी का ! बऊ भीतर पिघल उठीं।
सिर पर हाथ फेरती हुई बोलीं, ‘‘मुँह पोंछ डालो बेटा।’’
उसकी अधमुँदी पलकों के बीच पुतलियाँ चैतन्य नहीं हो पा रहीं। नींद का गहरा प्रभाव है। कुछ देर ऊँघती हुई बैठी रही। सिर दोनों बाँहों और घुटनों पर टिका लिया।
बऊ ने फिर हटोका, ‘‘उठो बिन्नू।’’
मन्दाकिनी पलकें मूँदें हुए ही बोली, ‘‘बऊ, आ गया श्यामली ?’’
‘‘और क्या ! आ नहीं गया !’’
‘‘उतरें बऊ ?’’ कहते हुए उसने अपनी सीपी-सी आँखें खोल दीं।
‘‘लो, इतेक देर से हम और क्या कह रहे हैं। पर पहलें अपनी फिराक-ठीक-ठाक कर लो।’’
बऊ ने बच्ची का कंधा थपथपा दिया।
वह खड़ी हो गयी। अपनी हरे रंग की फ्रॉक झाड़-झूड़कर नीचे को सरका ली। खेस के नीचे से नीली पट्टी वाली हवाई चप्पल निकालीं, पहनकर खड़ी-खड़ी, हाथ फेर-फेरकर अपने बालों को ठीक करने लगी। ज्यों कंघी से ओंछकर एक-से कर रही हो।
उधर के पहिये पर पाँव टिकाकर बऊ उतरीं और इधर की ओर मन्दाकिनी। बऊ कुछ देर तक लम्बी कद-काठी के चलते अकड़ी हुई कमर को सीधी करने के यत्न में खड़ी रहीं। फिर पाँवों में पहने चाँदी के लच्छे, जो आपस में उलझ-से गये थे, ठीक से बिठाये।
गनपत ने दोनों बैलों के रस्से नीम के तने से बाँध दिये। पिछौरा बँधा चारा उनके सामने खोलकर रख दिया और गाड़ी को जुआ झुकाकर एक ओर टिका दिया। अपना अँगोछा कंधो पर डालकर वे हाथ से पसीना पोंछते हुए बैलों के पास ही जमीन पर जा बैठे।
उनके बैठते ही बऊ कड़क आवाज में बोलीं, ‘‘द्वार खटकाओ गनपत।’’
अपनी आवाज में समायी बुलन्दी पर उन्हें स्वयं अचरज हुआ। लगा कि वे तो आज उसी लय में बोल रही हैं, जैसे अपनी बाखर में मईदारों को हुक्म सुनाया करती थीं और जिसे कुछ समय से भूलती जा रही हैं।
मन्दाकिनी ने निगाह घुमा-घुमाकर चारों ओर देखा। वीरानी को देखकर पूछने लगी, ‘‘यहाँ तो कोई नहीं है बऊ ! तुम तो कहती थीं, पंचमसिंह दादा के घर में बहुत-बहुत सारे लोग हैं !’’
बऊ ने अपनी धोती का पल्ला अच्छी तरह से कमर में खोंसा, नरम आवाज में बताने लगीं, ‘‘खेत कटनईं के दिन हैं बेटा, सब जने खेतों, खलिहानों में होंगे। घर की जनी-मानसें भी रोटी-पानी लैकें वहीं गयी होंगी।’’
बच्ची दो क्षण कुछ सोचती रही, सहसा चुप्पी तोड़ते हुए बोली, ‘‘हमारा खेत तुमने क्यों नहीं कटवाया बऊ ? कौन कटबायेगा। ?’’
बऊ के भीतर पैनी धार उतर गयी, क्या उत्तर दें इस प्रश्न का ? दो पल निरीह-सी देखती रहीं, फिर गहरा श्वास भरती हुई कहने लगीं, ‘‘भगवान कटबायेगा अब। अब उसी पनमेसुर के ऊपर छोड़ा है।’’
दादी का सूक्त वाक्य सम्भवतः बच्ची की समझ में नहीं आया। वह उन्हें उसी तरह प्रश्नवाचक नजरों से देखती रही।
कलईपुती दीवारें। किशमिशी रंग की चिकनी और पीतल की पीली कील-ठुकी किवाड़ें। मन्दाकिनी छू-छूकर देखने लगी।
घने नीम के हरियल वृक्ष की ओर देखती हुई बोली, ‘‘बऊ, अपने द्वार जैसा ही लग रहा है न इस घर का द्वार ?’’
बऊ ने ‘हाँ’ कहते हुए सिर हिलाया और महीन-सी हँसी हँस दी—‘‘सारे जमींदारों की हवेलियों की गढ़त एक-सी होती है स्यात।’’
दुबारा-तिबारा किवाड़ें भड़भड़ाने पर भारी चरमराहट के साथ द्वार खुला। किवाड़ों के बीच एक महिला खड़ी दिखाई दीं।
वे साँवली रंगत और मझोले कद की हैं। बीच की उम्र है। तरुणी न वृद्धा। हरी फूलदार किनारी वाली गुलाबी रंग की धोती पहने हुए। घूँघट माथे तक है। गले में सोने की हँसुली चमक रही है। बऊ ने उन्हीं पल-छिनों में सारा कुछ देख लिया।
‘‘सीताराम !’’ गनपत ने उनसे झुककर अभिवादन किया।
‘‘खुसी रहो, कहाँ सेऽऽऽ ?’’ उनका एक हाथ किवाड़ पर टिका था।
‘‘सोनपुरा से। महेन्दरसिंह की मतारी हैं हमारे संग। उनकी बिटिया मन्दा भी।’’ गनपत ने तर्जनी से इंगित कर दिया।
सुनकर एक पल को महिला का मुख विवर्ण हो आया।
कुछ देर अवाक् खड़ी रहीं।
जब सँभलीं तो पूछा, ‘‘जो मर गये थे, वे ही महेन्दरसिंह ? वे, जिनकी जनी...’’
गनपत ने स्वीकृति में सिर हिलाया।
‘‘दइया !’’ उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा।
बाहर की ओर गौर किया तो देखा कि कुछ दूरी पर एक वृद्धा, लगभग बारह-तेरह वर्ष की बच्ची को अपने से सटाये खड़ी हुई हैं। उनका हाथ बच्ची के सिर पर है और स्वयं कुछ। झुकी हुई-सी।
अभिवादन करने के लिए वे आगे बढ़ीं और बऊ के चरणों में झुक गयीं।
अधबीच ही रोक लिया बऊ ने। कंधे पकड़कर ऊपर उठा लिया।
‘‘पाँव जिन छुओ। रिस्ते में तुम हमारी भतीजी लगती हो। पंचमसिंह के घर से ही हो न ? देवगढ़वारी ?’’
‘‘हओ।’’
‘‘हम तुम्हारे पिता की फुआ की बेटी हैं, और यह हमारी पोती।’’ कहकर बऊ ने मन्दाकिनी को हाथ पकड़कर आगे कर लिया।
‘‘भीतर आ जाओ।’’ वे दोनों आगे हो लीं।
पौर में खटिया नवाती हुई सोच में बिंध गयीं, दादा ने तो इनकी आवाजाई को लेकर कुछ कहा नहीं। क्या करें ? क्या दुआरे से ही वापिस कर दें, या अपरिचित बनी रहकर किवाड़ें मूँद लें ? अब जो भी हो, द्वार आयी पाहुनी हैं। स्यात रहना भी हो इन्हें यहाँ, कि जाना हो....
खटिया बिछी तो बऊ बैठ गयीं। मन उठंग है। अधबीच लटका हुआ। मन्दाकिनी सहमी-सी एक ओर खड़ी अपनी लाल रिबन बँधी मोटी चोटी से खेल रही है।
वे बच्ची के पास पहुँच गयीं, ‘‘सरमा रही हो तुम ? हम कक्को हैं। घर-गाँव के सब लरका-बिटिया हमें ‘कक्को’ कहकर बुलाते हैं, तुम भी कक्को कहो।’’ उन्हें मन्दाकिनी को देखकर ममता उमड़ आयी। उसकी पीठ को सहारा देती हुई वे खटिया तक ले आयीं और अपने से सटाकर बिठा लिया।
वे देखती रहीं, बच्ची की आँखें कजरारी, घनी लम्बी बरौनियों वाली हैं, जिन्हें वह पटर-पटर झपका रही है। खाने वाला मुँह छोटा है, ऊपर का होंठ धनुष की तरह कटावदार और ललामी लिए हुए। मुख पर झलकती उम्र के मुकाबले कद लम्बा है। टेढ़ी माँग निकालकर बाल सँवारे हैं और एक लट अंडे की सी बनगत वाले चेहरे पर बार-बार झूल जाती है, जिसको सिर झटककर वह पीछे कर लेती है।
‘‘बहू जा बिटिया को छोड़कें चली गयी।’’ वे बऊ से मुखातिब हुईं।
बऊ कुछ न बोलीं, जैसे चुप्पी के परदे में स्वयं को छिपा रही हों।
‘‘पानी ले आवें हम। प्यास लगी होगी।’’ कहकर वे भीतर चली गयीं।
मन्दाकिनी खटिया पर बैठी-बैठी अपने लटके हुए पावों को हिलाने लगी थी, ज्यों पंजों को झूला झुला रही हो।
बऊ ने देखते ही हटोका, ‘‘सूधें बैठ जा मन्दा ! पाँव नहीं हिलाते, दोस होता है।’’
उसने अपने पाँवों की हरकत उसी दम रोक दी और पूछने लगी, ‘‘दोस क्यों होता है बऊ ?’’
बऊ से कोई उत्तर न बन पड़ा।
कक्को ने पानी भरा लोटा बऊ को थमा दिया। बऊ ने पानी का रंग देखा और बोलीं, ‘‘जे तो सरबत है। इतेक हमसे नहीं पिबेगा। मन्दा भी इसी में पी लेगी। और जिन लाना।’’
‘‘हमारे गनपत कक्का पियेंगे लाओ हम दे आयें,’’ मन्दा ने कहा—
वे विहँस उठीं, ‘‘तुम काहे ? हम दे आते हैं।’’
कक्को खटिया के पायँते बैठ गयीं। अब क्या बातें करे ? किस छोर की गहें ? कहाँ से आरम्भ करें ? और कहाँ अन्त ? दुख-विपता की बातें चलाना क्या आसान काम है ? जबकि मालूम हो, सामने बैठा मनिख ठहरी हुई पीर में फिर बहने लगेगा।
किस हिम्मत से छेड़ें बऊ के दुख का प्रकरण...वे चुप बैठी रहीं।
बातें बऊ से भी नहीं बन पा रहीं। पराया गाँव। बिरानी माँटी। अनचीन्ही धरती और अजनबी आसमान...जिधर को दृष्टि जाती है, अलगाव-सा झरता दीखता है।
बऊ गुमसुम बैठी रहीं।
देखती रहीं, मन्दा का मुख मलिन है। बाल उलझे हुए। फ्रॉक पर जगह-जगह मटमैले धब्बे लगे हैं।
उसका ध्यान भी अपनी फ्रॉक पर है।
बऊ ने गरदन में हाथ डालकर, कान के पास मुँह ले जाकर कहने लगी, ‘‘उठो बऊ, बक्सा खोलो। हम कपड़ा बदलेंगे।’’
उन्होंने धीरे से उसका हाथ दबा दिया, ‘‘अबै नहीं। तनक गम खाओ। रुकने-बैठने का ठौर...’’
अब वे दोनों बरामदे में खेस बिछाकर बिठा दी गयीं।
‘‘बऊऽऽ !’’ मन्दाकिनी ने अपनी फ्रॉक दिखाकर फिर ध्यान दिलाया।
‘‘मन्दा, तुम भी बड़ी जिद्दिन हो। कह तो रहे हैं, अबै कहाँ से निकार दें तुम्हारे उन्ना कपड़ा ? कित्तै धर के खोलें बक्सा ?’’ बऊ खीजी-सी फुसफुसाईं।
घर की स्त्रियाँ अपने कामों से फुरसत पाकर उनके पास आ बैठीं।
बातें चल उठीं। मिल-जुलकर उसी विपत्ति की परतें उखाड़ी जाने लगीं, जिससे वे कतई बचना चाहती हैं।
‘‘लो भाग तो देखो कि इतेक मुसीबत।’’
दूसरी बोली, ‘‘भाग-कुभाग की क्या बात, इनकी बहू ने ही संग नहीं दिया, तो फिर कोई गैर कैसे समझेगा इनकी पीर ?’’
मन्दाकिनी देख रही है, इन औरतों के गोदों में बच्चे हैं। छाती से दूध चूसते हुए बच्चे। गोदी में बैठकर खुश होने वाले बच्चे। एक-दो गोद में बैठकर भी रोने वाले बच्चे, जिन्हें वे अनजाने की थपथपा देती हैं और छूटी हुई बात का छोर गहकर बऊ को फिर खींच लेती हैं चर्चा में।
‘‘जीजा के संग भग गयी।’’ एक ने कहा।
‘‘भग कहाँ गयी अपहरन हुआ है बेचारी का।’’ दूसरी ने तर्क दिया।
‘‘अई, नोंनें रहो। अपहरन काहे ! अपहरन होता तो बऊ का न हो जाता। जे भी तो भर ज्वानी में विधवा हुई थीं। जे कहो कि मस्तानी हती। ज्वानी की मारी। सो बिना खसम के रहाई नहीं आयी।’’
बऊ की भीतरी परतें छिलने लगीं। सुनते-सुनते आँखों में नमी आ गयी। मन्दाकिनी कुछ देर तक उन औरतों को घूरती रही। उसके होंठ भिंच गए, आँखें बड़ी और पनीली-सी दिखने लगीं। बऊ को अधिक उदास देखकर उनके घुटने पर अपना सिर टिका दिया।
सहसा वे सब द्रवित-सी हो गयीं, बोलीं, ‘‘देखो तो, मोंड़ी हिंरस उठी। कैसी कठकरेज मतारी हती कि छोड़ गयी पुतरिया-सी बिटिया कों ! चिरइया-परेबा तक नहीं छोड़ते अपने अंडी-बच्चा।’’
साँझ हो आयी।
आँगन में धूप सरककर दीवारों पर पहुँच गयी।
एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण मन्दाकिनी ऊबने लगी। बऊ को संकेतों से समझाने लगी कि चलो बऊ।
वे अनदेखा किये बैठी रहीं। दादा की प्रतीक्षा है उन्हें। आ जाते तो रुख का पता चलता। भले ही सहमति है, लेकिन उनका सन्देही मन कई तरह से सोचने लगता है। न जाने किस तरह से लें उनके आने को ? हँसी-खुशी में पाहुनी बनकर थोड़े ही आयी हैं, संकटों में उलझी आगन्तुका हैं। ऐसे में कौन कर सकता है स्वागत ? अपने ही किनारा कर जाते हैं दुख-तकलीफ के बखत।
फिर दादा कहीं यह न सोचने लगें कि मातौन तो आदर के भी खा गयीं। हमने झूठे को कहा और वे साँचे को चली आयी।
दिन डूबने में जो घंटा-डेढ़ घंटा बचा है, वह उन्हें बहुत लम्बा और भारी लग रहा है। काटे नहीं कट रहा।
मन्दाकिनी की दृष्टि अब कहीं और है।
स्कूल से बच्चे लौट चुके हैं। माँओं से खाने की माँग कर रहे हैं। कक्को से घी और चीनी के लिए जिद कर रहे हैं। सब्जी देखकर मुँह बिचका रहे हैं।
कुछ बस्ते रखकर पनारे पर मुँह-हाथ धोने में लगे हैं।
उसे अजनबी निगाहों से देख रहे हैं। अनचीन्हे भाव से घूर रहे हैं।
उसने अपनी फ्रॉक के घेर को घुटनों से खींच-खींचकर दोनों टाँगें ठीक प्रकार ढक लीं और खेस के ऊपर भली प्रकार बैठ गयी।
बऊ बोलीं, ‘‘तुम ज्यादा न तानना फिराक को, फट जायेगी।’’
कतार बनाकर बोरियाँ डाली गयीं। परसी हुई थालियाँ उनके आगे रखी गयीं। थालियों में आलू-बैगन का साग, दही का कटोरा, घी से चुपड़ी हुई ठंडी रोटियाँ। मिर्च और आम का अचार।
बच्चों ने मिलकर स्वर साधा :
‘‘आलू भटा की तिरकाई, नाचे मुन्ना की मताई।’’
फिर सब हँस पड़े।
मन्दाकिनी खिलखिलाती हुई पीछे तक हँसती रही।
सबका ध्यान उसकी हँसी पर ठहर गया।
वह एकदम चुप हो गयी।
कक्को ने उसे हाथ पकड़कर उठा लिया, ‘‘चलो, तुम भी खा लो।’’
अपनी पंक्ति में उसे बैठे हुए खाते देखकर लड़के विचित्र भाव से हँसने लगे। आपस में कान पर मुँह रखकर कुछ कह रहे हैं, जिसे वह सुन तो नहीं पा रही, लेकिन समझने की कोशिश कर रही है।
इस तरह का व्यवहार उसे बिलकुल अच्छा नहीं लगा। थाली लेकर जल्दी ही उठ गयी और पनारे पर रख आयी।
लौटकर बऊ के पास आ बैठी। बेचिन्हारा स्थान, अपरिचित चेहरे जैसे उसे दुखी और तंग करने पर तुले हैं। उसे सुगना की याद आने लगी। सात-आठ साल की सुगना उसके साथ ही साथ लगी रहती थी। स्कूल से लेकर तालाब-पहाड़ सब जगह संग। सुगना की चोटी से खोलकर यह लाल रिबन काकी ने चलते समय उसकी चोटी में बाँध दिया था। हड़बड़ी में कंघी-रिबन मिले ही नहीं थे उसे। बऊ ताला लगाने की जल्दी जो मचा रही थीं।
वह गाड़ी में बैठकर चली थी तो सुगना रोने लगी थी। जगेसर कक्का ने डपट दिया था काकी को कि चलो अपने घरै। आँखों में आँसू भरे सुगना कभी पिता की ओर देखती, कभी उसकी ओर।
‘‘बऊ, सुगना के पिता जी हैं, जगेसर कक्का। पिता जी हैं तो हर समय डाँटते क्यों रहते हैं ?’’
बऊ कुछ न बोलीं।
वह रिबन को ही देख रही है। सुगना का गोरा मुख याद आ रहा है कि अचानक बच्चों के झुंड में से कोई स्वर सुनाई पड़ा :
‘‘एक फूल की चार कली, रानी डोले गली-गली।’
ये क्या चिढ़ा रहे हैं उसे ? और नहीं तो क्या ? उसने मारे गुस्से के उन शैतान बालकों की ओर से पीठ कर ली। तमतमाई-सी बैठी रही।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book