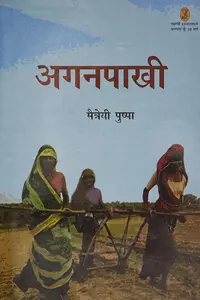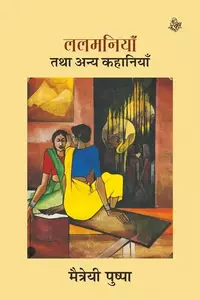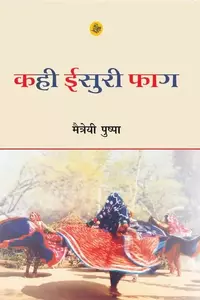|
कहानी संग्रह >> चिह्नार चिह्नारमैत्रेयी पुष्पा
|
27 पाठक हैं |
|||||||
मैत्रेयी पुष्पा की तेरह कहानियों का संग्रह
Chinhaar
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘‘माँ, लगाओ अँगूठा !’’ मँझले ने अँगूठे पर स्याही लगाने की तैयारी कर ली, लेकिन उन्होंने चीकू से पैन माँगकर टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में बड़े मनोयोग से लिख दिया-‘कैलाशो देवी’। उन्हें क्या पता था कि यह लिखावट उनके नाम चढ़ी दस बीघे जमीन को भी छीन ले जाएगी और आज से उनका बुढ़ापा रेहन चढ़ जाएगा।
रेहन में चढ़ा बुढ़ापा, बिकी हुई आस्थाएँ, कुचले हुए सपने, धुँधलाता भविष्य-इन्हीं दुःख-दर्द की घटनाओं के ताने-बाने से बुनी ये कहानियाँ इक्कीसवीं शताब्दी की देहरी पर दस्तक देते भारत के ग्रामीण समाज का आईना हैं। एक ओर आर्थिक प्रगति, दूसरी ओर शोषण का यह सनातन स्वरुप ! चाहे ‘अपना-अपना आकाश’ की अम्मा हो, ‘चिन्हार’ का सरजू, या ‘आक्षेप’ की रमिया, या ‘भँवर’ की विरमा-सबकी अपनी-अपनी व्यथाएँ हैं, अपनी-अपनी सीमाएँ!
इन्हीं सीमाओं से बँधी, इन मरणोन्मुखी मानव-प्रतिमाओं का स्पंदन सहज ही सर्वत्र अनुभव होता है-प्रायः हर कहानी में।
लेखिका ने अपने जिए हुए परिवेश को जिस सहजता से प्रस्तुत किया है, जिस स्वाभविकता से, उससे अनेक रचनाएँ, मात्र रचनाएँ न बनकर, अपने-अपने समय का, अपने समाज का एक दस्तावेज बन गई हैं।
रेहन में चढ़ा बुढ़ापा, बिकी हुई आस्थाएँ, कुचले हुए सपने, धुँधलाता भविष्य-इन्हीं दुःख-दर्द की घटनाओं के ताने-बाने से बुनी ये कहानियाँ इक्कीसवीं शताब्दी की देहरी पर दस्तक देते भारत के ग्रामीण समाज का आईना हैं। एक ओर आर्थिक प्रगति, दूसरी ओर शोषण का यह सनातन स्वरुप ! चाहे ‘अपना-अपना आकाश’ की अम्मा हो, ‘चिन्हार’ का सरजू, या ‘आक्षेप’ की रमिया, या ‘भँवर’ की विरमा-सबकी अपनी-अपनी व्यथाएँ हैं, अपनी-अपनी सीमाएँ!
इन्हीं सीमाओं से बँधी, इन मरणोन्मुखी मानव-प्रतिमाओं का स्पंदन सहज ही सर्वत्र अनुभव होता है-प्रायः हर कहानी में।
लेखिका ने अपने जिए हुए परिवेश को जिस सहजता से प्रस्तुत किया है, जिस स्वाभविकता से, उससे अनेक रचनाएँ, मात्र रचनाएँ न बनकर, अपने-अपने समय का, अपने समाज का एक दस्तावेज बन गई हैं।
दूसरे संस्करण पर
मैं भूमिका लिखने के पक्ष में नहीं हूँ, ऐसा दावा भला कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि ‘चिह्नार’ और ‘बेतवा बहती रही’ इन दोनों पुस्तकों की भूमिका लिख चुकी हूँ, और अब ‘चिह्नार’ के दूसरे संस्करण पर फिर....। वैसे भूमिका लिखना पाठक को रचना की ऐसी कुंजी पकड़ाना है, जो उसका विवेक छीनकर ताला अपने ढंग से खोलने का संकेत देती है।
....लेकिन यहाँ मेरा इस तरह का कोई इरादा नहीं। केवल पहले-पहल की कहानियों के पात्रों के मनोभावों की भूमि तैयार करने के प्रति एक स्वीकरोक्ति है, जिसे देने की इच्छा बार-बार जागती रही।
दरअसल पहले-पहल जब लेखक का साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश होता है, तो वह शब्द की विराट दुनिया को चकाचौंध होकर देखता है। वह कहाँ खड़ा है, इससे बेखबर-सा। लिखने की चुनौतियों से ज्यादा अपना नाम छपा देखकर विभोर हो जाता है। कुछ भ्रम भी पाले रहता है—पाठक को प्रभावित करने के लिए। पता नहीं औरों के साथ ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ—करुणा के साथ दया, संवेदना के साथ तरस और अभिव्यक्ति को तरल भावुकता में सानकर छायावादी भाषा के सहारे लिखने लगी—सांस्कृतिक तत्सम शब्दों के व्यामोह से पीड़ित, लेकिन एक छोटी-सी ताकतवर लौ के साथ, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अँधेरे को चीरकर मानवीय मूल्यों को झलका सके, जगमगा सके।
कालक्रम के हिसाब से कहूँ तो मैं बहुत जल्दी ही महसूस करने लगी कि कहानी का मुहावरा बदल जाना चाहिए। निष्ठुर समय से टकराने के लिए अपने दूसरे कहानी संग्रह ‘ललमनियाँ’ तक आते-आते लिखावट के तेवर धारदार लेकिन ठंडी भाषा अख्तियार करते चले गये, जो गर्म लोहे की तरह लचकने से बच सकें।
‘चिह्नार’ की कहानियों के बारे में चर्चा करते हुए हंस-संपादक श्री राजेन्द्र यादव ने कहा था, ‘‘तुमने इन दस्तावेजों में अनुभवों की बहुमूल्य पूँजी को बेदर्दी से खर्च किया है।
....लेकिन यहाँ मेरा इस तरह का कोई इरादा नहीं। केवल पहले-पहल की कहानियों के पात्रों के मनोभावों की भूमि तैयार करने के प्रति एक स्वीकरोक्ति है, जिसे देने की इच्छा बार-बार जागती रही।
दरअसल पहले-पहल जब लेखक का साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश होता है, तो वह शब्द की विराट दुनिया को चकाचौंध होकर देखता है। वह कहाँ खड़ा है, इससे बेखबर-सा। लिखने की चुनौतियों से ज्यादा अपना नाम छपा देखकर विभोर हो जाता है। कुछ भ्रम भी पाले रहता है—पाठक को प्रभावित करने के लिए। पता नहीं औरों के साथ ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ—करुणा के साथ दया, संवेदना के साथ तरस और अभिव्यक्ति को तरल भावुकता में सानकर छायावादी भाषा के सहारे लिखने लगी—सांस्कृतिक तत्सम शब्दों के व्यामोह से पीड़ित, लेकिन एक छोटी-सी ताकतवर लौ के साथ, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अँधेरे को चीरकर मानवीय मूल्यों को झलका सके, जगमगा सके।
कालक्रम के हिसाब से कहूँ तो मैं बहुत जल्दी ही महसूस करने लगी कि कहानी का मुहावरा बदल जाना चाहिए। निष्ठुर समय से टकराने के लिए अपने दूसरे कहानी संग्रह ‘ललमनियाँ’ तक आते-आते लिखावट के तेवर धारदार लेकिन ठंडी भाषा अख्तियार करते चले गये, जो गर्म लोहे की तरह लचकने से बच सकें।
‘चिह्नार’ की कहानियों के बारे में चर्चा करते हुए हंस-संपादक श्री राजेन्द्र यादव ने कहा था, ‘‘तुमने इन दस्तावेजों में अनुभवों की बहुमूल्य पूँजी को बेदर्दी से खर्च किया है।
अपना-अपना आकाश
यहाँ रहते हुए उन्हें चार महीने हो चुके थे, यह वे भी जानती थीं। पन्द्रह दिन पहले से मन में जोड़-गाँठकर हिसाब लगा रही थीं, इसकी वे अभ्यस्त हो चुकी थीं। अब फिर दिल्ली जाना था बड़े बहू-बेटों के पास...। दिल्ली के नाम से उनकी रूह थरथराने लगती थी, एक मुकम्मल दहशत जो मन में बैठ गई थी। जीवन का एक-एक दिन उनके लिए भारी हो उठा था, लेकिन अपने आप क्या कोई प्राण तज सकता है....?
वे उठना चाहती थीं, पर उठते समय लग रहा था जैसे हाथ-पाँवों का अंश खिंच गया है—अब इतना जाघर कहाँ था कि झमककर उठ पड़ें। कोई उमंग उछाह हो तो बूढ़े हाथ-पाँव भी त्वरित गति से चलने लगते हैं, मन में हील-हुलस ही नहीं तो तन भी शिथिल हो जाता है। जाने के नाम से उन्हें झुरझुरी चढ़ने लगी थी और शरीर में ठीक बुखार के पहले की-सी टूटन। सामान तो रखना ही था, वे बेबस सी उठ खड़ी हुईं। अलगनी पर टँगे अपने कपड़े बटोर लाईं पर उन्हें तहाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, कमरे में पड़ी खाट पर तन ढीला छोड़ बेदम-सी बैठ गईं। लग रहा था माथे के भीतर चक्रवात उठ रहे हैं और कानों में सनसनाहट। कुछ देर बाद खिड़की से बाहर झाँकने की शक्ति बटोर वे खिड़की पर खड़े हो पुकारने लगीं—
‘‘नीटूऽऽऽ अरी नीटूऽऽऊ !’’
‘‘हाँ अम्मा !’’ छोटी पौत्री ने अपने खेल में व्यवधान डाले बिना ही उत्तर दिया।
‘‘अरी यहाँ आ री मेरे झौरें !’’ वे बुलाने लगीं।
लेकिन नीटू नहीं आई, वहीं कंधे उचकाकर रह गई। वे एक-दो बार और आवाज देती रहीं लेकिन नहीं—नीटू नहीं आई। वे खिसियायी-सी अपने कपड़ों को तह करने लगीं। दवा निकालकर रख ली, उसी के लिए पानी माँगना चाहती थीं, लेकिन....मग्धड़ छोकरी।’ वे बुदबुदा उठीं। फिर स्वयं ही जाने को तत्पर हुईं कि बहू गिलास में पानी लेकर हाजिर हो गई। जब यहाँ से जाने का वक्त समीप आता जाता तो बहू अति आर्द्र हो उठती, यह बात वे जानती हैं। दो-चार रोज बहू बड़ी मुस्तैदी से उनकी आज्ञा का पालन करती है, चीजें पल-छिन में हाजिर कर देती है। पर नीटू अभी कहाँ जानती है कि कब अपने व्यवहार में फेर-बदल कर देनी चाहिए ! कभी-कभी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होने लगता है कि इतनी अवस्था जी लेने के बाद भी वे वह सब क्यों नहीं सीख पाईं जो कल की छोकरी इन बहुओं ने गुन लिया। वे कैसी नारियल-सी बनी रहीं, ऊपर से चिकनाई मलना उन्हें जिन्दगी-भर क्यों नहीं आ पाया ?
‘‘अम्मा जी, बाँधि लियौ सामान ?’’ इस घर का नौकर लल्लू पूछ रहा था।
‘‘आजु राति कूँ ही जानौ है, जरूली भइया ?’’ वे अनुनय-सी करती पूछने लगीं कि शायद उनका जाना कुछ दिन और टल जाय।
‘‘देखि लेउ, फिर मेरी फुस्सित नाँय। टैम तो तुम्हारौ हू पूरौ है गयो यहाँ।’’ लल्लू अपनी मजबूरी जताते हुए यहाँ के अनुबन्ध की याद दिलाने लगा।
जाना तो पड़ेगा ही—वे सोचने लगीं और अटैची में हाथ से तहायी दो-चार धोती, ब्लाउज, पेटीकोट निरपेक्ष भाव से डालने लगीं। पर क्या करें, मन बार-बार हिलककर रह जाता वाक्यों की डोर से—
‘‘अम्मा, लखिया आबैगो। कचहरी में तारीख है, सो अम्मा, चाहें दुबक कें ही सही, तुमते मिलि कें जरूल जायगो।’’ गाँव से आया नाई उनसे कह गया था।
पर अभी लखिया की दी हुई तारीख में तो आठ दिन बाकी थे, इतना कौन रुकने देता उन्हें यहाँ। वैसे लखिया से मिलने का जतन तो उन्होंने खोज लिया था। चौराहे से दायें हाथ को जाने वाली गली का मंदिर भी बता दिया था नाई को, कि वे लखिया को उस मंदिर में मिल जाएँगी, पर अब कैसे...? मन में अटूट बेचैनी समेटे वे बहुत देर तक चुप्प अडोल-सी खाट पर बैठी रहीं।
छोटी बहू जल्दी-जल्दी खाना बना रही थी उनके साथ रखने के लिए। ‘‘रेलगाड़ी का खाना अम्मा कैसे पचा पाएँगी, सो जो उन्हें पसन्द है वही बना दिया है, कम-से-कम खा-पीकर तो पहुँचेंगी उनके घर।’’ बहू-बेटे की बतलावन वे साफ सुन रही थीं। इस बहू में कुछ सीमा तक तो सौहार्द्रता है। दिल्ली वाली बहुएँ तो कुछ ज्यादा ही तिनख हैं, वे उनकी बूढ़ी ठूठ काया की सामर्थ्य-असामर्थ्य नहीं पहचानना चाहतीं। तभी न उस दिन बड़ी बहू ने हुक्म सुना दिया था—
‘‘अम्मा जी, आज तो बच्चे चायनीज खाने की जिद कर रहे थे सो उसी में से आया आपको भी दे देगी, खा लेना।’’कहकर बहू पर्स झुलाती हुई घर से बाहर निकल गई। कैसे-कैसे खा पाई थीं उस अजब से भरछत भोजन को। नोन-मिर्च कि सिवई तो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं। इतने बड़े जीवन में सिवइयों को उन्होंने हमेशा घी-बूरे के साथ परोसा था। नूडल्स पेट में डाल तो लिये लेकिन खाते ही पेट फुँक गया था। सिरका और मिर्च के जोड़ ने बूढ़ी आँतों को जला डाला था। अगले दो दिन तक मरोड़ और दस्तों से पीड़ित रही थीं। दोनों बहुएँ फुसफुसा उठी थीं—‘‘देखती नहीं कितना पचा पाएँगी, बस खाए सिद्ध।’’
स्टेशन छोड़ने बेटा-बहू दोनों आए थे। वे चलते समय नीटू और बबली के हाथ पर पाँच-पाँच रुपये रख आई थीं, बहू उन्हें ही लौटा रही थी—‘‘अम्मा जी, आप ही रख लो, आपके काम आएँगे, बच्चों को क्या कमी है।’’
‘‘अरी बच्चन के हाथ पर धर दीजो।’’ कहकर वे मन में कहीं उमेठ महसूस करने लगीं...अकथनीय पीड़ा से अन्दर ही अन्दर तिलमिलाकर रह गईं।
ट्रेन सीटी दे चुकी थी। लल्लू उनकी अटैची और नाश्तेदान थामे उन्हीं के पास आ बैठा था हमेशा की तरह। बेटे ने पैर छुए, उसके बाद बहू ने—‘‘बेटा होय...खाने अघाने रहौ....’’ आशीष देकर वे एक पल को अनचाहे ही आनन्दित हो उठी थीं सब कुछ भूलकर। फिर मन भारी हो उठा, आँखें भर आईं थीं। लेकिन उनसे छुटकारा पाने की जो अतिरिक्त उत्फुल्लता बहू के मुख पर चमक रही थी उसे देख वे अपनी अवांछनीयता पर संतप्त हो उठीं। वे रोना नहीं चाहती थीं फिर भी आँसू आँखों में छितराकर एक धुन्ध-सी छोड़ गए दृष्टि के सामने।
गाड़ी सरक ली थी और शहर से दूर होते उन्हें लग रहा था जैसे वे बेगानेपन के बियाबान में भागती हुई अनन्त रेगिस्तान की ओर जा रही हैं। जहाँ कोई अपना था न आत्मीय....।
‘‘लखिया आवैगो पर लौट जाइगो कम्बखत, ‘वे अपने-आप में ही बुदबुदा रही थीं। अपनी पराश्रिता पर क्रोधित थीं वे। बेटों के कहने से क्यों गाँव छोड़ा ? क्यों अपनी देहरी का मोह तज ममता की मृग-मारीचिका के पीछे भाग लीं, या डर गई थीं वे ? फिर क्यों नहीं दृढ़ होकर खड़ी हो सकी थीं बेटों के समक्ष ? यह वे स्वयं नहीं आज तक जान पायीं। ममता, भय और रक्त का आपसी मेल-जोल खींच लाया था उन्हें यहाँ। अपने मनोबल की कमी पर तब से अब तक पछताती रही हैं। लखिया तो पैरों से लिपटा कैसा हिलककर रोया था—‘‘भाभीऽऽऽई, तू मत जाऽऽय भाभीऽऽऽई...।’’
क्या उत्तर देतीं इस बेजार हूक का, बैलगाड़ी में बैठी सिसकती रही थीं। सिर का पल्ला नीचे सरका लिया था। आधे घूँघट में ही बूढ़ी आँखें बरसती रही थीं, बेटों की सोच का क्या भरोसा ? कलेजे में उठी सुबकी गले में ही घुँटती रही थीं।
वे जिस द्वार-चौखट को छोड़े जा रही थीं, उस घर में सास मरने के कुछ दिन बाद ही ब्याह के आ गई थीं और नववधू का जामा उतार ठेठ घरनी बनी गृहस्थी के उस कठिन प्रश्न-पत्र को हल करने में लग गईं जिसे उनकी सास अधूरा छोड़ गई थीं। जैसी आकांक्षा—वैसा ही परिणाम....वे सास से चार हाथ आगे ही निकली थीं। गृहस्वामिनी के अभाव में जो घर करब के झुये-सा बिखरा जा रहा था उसे उन्होंने तुरन्त बाँहों में भरकर प्रेम-रज्जु से कसकर बाँध दिया था।
वे पखेरुओं के कलरव से पहले उठ जातीं। घर बाहर की झाड़ू-बुहारी, पानी-लत्ता और लीपा-पोती से लेकर ढोर-डंगरों की सानी-पानी सब कर डालतीं। ससुर के लिए दातुन और पानी से भरा सोने-सा दिपदिपाता जगन्नाथी लोटा मोरी पर धर देतीं, झटककर लखिया को जगा लातीं—‘‘सूरज मूड़ पै चढ़ौ है और तुम खटिया पर परे सोइ रहे। उठौ, कुल्ला-दातुन करौ।’’
लखिया कैसा अल्हड़ बछेड़ा-सा मिला था उन्हें, इधर-उधर उजबक-सा फिरता, पाँवों पर ओक बहाए। आँखों में कीचड़ और दाँतों पर पीलेपन की परत....। कुछ दिन तो लिहाज में चुप ही रही थीं—उम्र में छोटा है तो क्या—है तो देवर ही। पर उसकी बावरी वेश-भूषा और गंदेलापन वे ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाई थीं। प्यार से कहतीं तो वह सुनता ही कहाँ था, ज्यादा-से-ज्यादा धुली कमीज पहनकर सिर पर टोपी धर लेता पर टाँगों में वही पट्टे का घुटन्ना लटकाए पूरे गाँव में चकफेरी करता रहता, गिल्ली डंडा बजाता रहता। बड़ी मुश्किल से पाजामा पहनने की आदत डाली थी और कंच्चे-गुच्ची से छुड़ाकर तख्ती पकड़ाकर स्कूल को ठेला था, पर क्या वह तख्ती से आगे बढ़कर स्याही-कापी पकड़ पाया ? तख्ती-टाट पकड़े ही ओठों पर रेख निकल आई थी। हाँ, भाभी के वचन पालन करते-करते जरूर वह पालतू मेमने-सा हो उठा था।
घर में ससुर, विधुर चचिया ससुर, अनब्याहा जेठ, पति, लखिया और मेहनती मजदूरों की रेल-पेल—अच्छा-खासा कुनबा था और अकेली औरत जात—वे। रोटी सेंकने बैठतीं तो सुबह से दोपहर हो आती, पर वे जरा-सी भी तो नहीं डगमगाती थीं कभी। उनकी सहजता देखकर क्या लगता था वे अपनी परिवार की नाजोंपली सबसे छोटी पुत्री होंगी, जिन्हें माँ और भाभियों ने तवे पर चँदिया नहीं डालने दी थी।
उनकी दक्षता देखकर ही तो ससुर ने कनस्तरी-भरे स्वर्ण-आभूषण उन्हें ऐसे सौंप दिए थे जैसे किसी विवाह-गृह से आया लड्डू-कचौड़ी का पड़ोसा हो, और वे उसे कभी उपलों में दाब आतीं, कभी अनाज-भरे गड्डे में गाड़ आतीं। तब बैंकों में रखने का चलन ही कहाँ था—सोचकर अपनी चतुराई पर वे स्वयं ही मुस्कुरा उठीं।
चतुर सुघड़ बहू सम्मान और सराहना की दावेदार थी। कारज-ब्यौहार, परव-त्योहार सबकी अग्रणी बनी रही थीं। समय कैसे सरग के पाखी-सा उड़ा गया, उन्हें खबर ही कहाँ लगी थी, वे तो भोर से साँझ और साँझ से भोर को जीवंत करती रहीं। इसी बीच वे तीन बेटों की माँ बन गईं। लखिया का ब्याह हो गया। लखिया का सम्बन्ध करते समय ससुर जी को उन्होंने कितना रोका था, पड़ौसी का लड़का बुलाकर उससे नाहीं करायी थी, तर्क दिलवाए थे कि लखिया को अभी शादी-ब्याह का क्या शऊर...। लेकिन—
‘‘अब का कल्ला फूटिंगे जा लखिया में,’’ कहते हुए ससुर जी हुक्का गुड़गुड़ाते चौपाल पर निकल गए थे।
जवान-जहान बहू घर पर आ गई तो लखिया कैसा दुबका-दुबका फिरा था। भाभी का पल्ला एक पल को नहीं छोड़ता था। हर काम तो उसने भाभी से पूछकर किया था, फिर अब कैसे...? उसकी भाभी-भक्ति देखकर कभी-कभी तो उन्हें ही खटका होने लगता—बहू क्या सोचेगी....? भाभी का चाकर उसका पति...कैसे बर्दाश्त करेगी ?
धकिया-पिछियाकर किसी तरह रात को बहू के पास भेजा था, पर वहाँ भी ढाक के तीन पात !
वे सवेरे ही बहू के पास जाना चाह रही थीं पर बार-बार हिम्मत बाँधने पर भी मन अड़ियल तुरंग-सा पीछे हटता ही चला जाता—कैसे पूछेंगी नई ब्याही से कि इस लखिया में मरदपने के लच्छन हैं कि नहीं ? वयस में वे बहू की कोई हमउम्र तो थीं नहीं। लेकिन चिन्ता रात-भर उन्हें दीमक-सा खाती रही थी, एक पल को पलक नहीं मूँद सकी थीं...उसी बेचैनीवश पूछ बैठी थीं रात की बात...। बहू खिलखिलाकर हँस पड़ी थी।
‘‘काहे को हँस रही है री बिन्दो....बता न !’’ वे स्वयं नई दुल्हन की तरह शरमा उठी थीं, नीची आँखें किए कपोलों पर लाली दौड़ गई थी।
‘‘जीजीऽऽई...जीजीऽऽ हऽहऽहऽहऽअ !’’ बिन्दो हँसी नहीं रोक पा रही थी।
‘‘अब कछु बोलैगी हू कै हसति ही रहेगी,’’ वे आतुरता से भर उठी थीं—‘‘बोल जल्दी।’’
‘‘जीजी, हऽऽअ हऽऽ ! जीजी, काहे को भेजि दीये तुमने ? पहले तो नीचे कू मुँह करें ठाड़े ही रहे, फिर हाल भये पिल्ला से कुँइ-कुँइ करि कें सोई गए। मैं झकझोरि-झकझोरि कें हारि गयी, अब तक नाहिं उठे। अब तुम हि जगाय लेउ जाय कें !’’
उन्होंने अपने माथे पर हाथ दे मारा—‘‘हाय मेरे राम जी !’’ वे क्या कहती बिन्दो से कि यह हौलू बिल्लाल निरा औघड़ है। अरे, खाना-पीना और यह सब...तो चिरई-चिरवा भी जानते हैं, फिर यह तो मानस-मनिख का पूतरा, कौन समझाए इस मूरख को ! वे अजीब-सी दुविधामयी चिन्ता से घिर उठी थीं। वह तो बिन्दो समझदार निकली कि बालक की तरह भाभी के पल्लू से बँधे पति के प्रति कभी रोष प्रकट नहीं किया।
सारे घर का काम उठा लिया था बिन्दो ने। अपनी जीजी को तो किसी काम से हाथ नहीं लगाने देती। लेना-देना, ऊपर का इन्तजाम और घर की मुख्तारी ही रह गई थी उनके जिम्मे। जिठानी के तीनों बच्चों का लालन-पालन भी बिन्दो ने अपनी ही गोद में डाल लिया था। वे पूजा करते-करते सौ-सौ बार ठाकुरजी को माथा झुकातीं कि हे मेर पिरभू ! लखिया के बचपन को हाथ लगाकर जरा-सा सगुना क्या दिया, मुझे बदले में ऐसी हिरदय की टूक सहोदरा बख्श दी !
मजाल है कि बिन्दो जीजी के बिना कौर तोड़ जाय। वे हजार बार कहतीं—‘‘अरी बिन्दो, खाय लै री ! कब तक भूखी बैठी रहैगी ?’’ पर वह दोनों का भोजन एक ही थाली में परोसकर बैठ जाती—‘‘आ जाऔ जीजी, अब बहौत है गयी पूजा। और कहा माँगि रही हौ राम जी पै। सब तौ है।’’ कहकर जोर से हँसने लगती। बिन्दो हरगिज ग्रास न तोड़ती जब तक कि वे तुलसी के चौरा पर लौटा न ढार लेतीं।
बहुत समय बीत गया था पर बिन्दो के गर्भ में आस नहीं ठहरी थी। मुहल्ले में खुसुर-पुसुर होने लगी थी। वे घबरा उठी थीं बहुत अधिक।
जब पहले-पहले बिन्दो के पाँव भारी हुए तो उन्हें लगा था वे ताई नहीं, दादी बनने जा रही हैं। हौंस-हुलस से भरी वे कृष्ण कन्हैया और यशोदा के गीत गाया करतीं। हाथोंहाथ रखतीं बिन्दो को; पर वह भी मरी बड़ी अड़ियल थी, न जाने कब खेत पर जाकर चौड़ी नाली का पाट फलाँग गयी। तबीयत बिगड़ी तो वे बैलगाड़ी में धरे इस डॉक्टर से उस डॉक्टर पर भागती रही थीं लेकिन कहाँ ठीक हो सका था...कच्चा ही गिर गया, बिन्दो ही बड़ी मुश्किल से बच पायी थी।
उनके पति को न जाने कौन-सा रोग लगा था कि गँवई-गाँव से लेकर शहर तक के इलाज़-उपचार हुए लेकिन वे एक दिन....और इसी तरह ससुर, चचिया ससुर मृत्यु-पथ पर अनुगामी बने चल दिए। अनब्याहे जेठ तो कब के साधू होकर चले गए थे। बड़ों का साया सिर से उठ गया। रह गए वे और लखिया, अनाथ हुए पूरी गृहस्थी का वजन लिए। पर लखिया समय का नाजुक मिजाज पहचानकर रातोंरात कैसे घर का पालनहार बनकर खड़ा हो गया कि वे स्वयं विस्मित रह गयी थीं। उनके तीनों बच्चों की पढ़ाई में रंचमात्र का अंतर नहीं आने दिया लखिया ने। भीषण लू-लपट और शीत सरकती रातों को बराबर करके वह बैलों के साथ बैल की नाईं जुतता रहता। रक्त-स्वेद मिलाकर धरती की कोख में बीज बोता रहा और फसल समेट-बेचकर भाभी के हाथ पर पाई-पाई रखता रहा। भतीजों को पढ़ा-लिखाकर योग्य बनाने का व्रत साध वह स्वयं धरती की धूल में मिलता रहा था।
आड़ा समय भी निकल गया अच्छे ही वक्त की तरह। तीनों बेटे बड़े हो गए। बड़े दोनों दिल्ली में नौकरी करने लगे, छोटा आगरा बैंक में मैनेजर हो गया। लखिया का श्रम सफल हो गया था। वे निछावर हो गयी थीं पुत्र-सरीखे देवर पर। शादी की बात आयी तो जाहिर है कितने ही धनाढ्य शहरी कन्याओंके पिता उनके बेटों के ससुर बनने का सौभाग्य खोजने लगे। उन पिताओं को योग्य दामाद चाहिए थे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं...। शादी भी उनके बेटों ने शहर में पली-पुसी कन्याओं से की, गाँव की अल्हड़ गँवार को वे कैसे निभा पाते ! शादी की बाबत बेटे ने माँ और चाचा को पूछा ही कहाँ ही था, बस खबर दे दी थी कि इस-इस तारीख को चले आयें, सो वे लखिया और बिन्दो को लेकर चली गयी थीं। गाँव आकर बड़े ताने-उलाहने सुनने पड़े थे—‘‘बेटा ब्याहि लियौ और एक खीकरी तक न दिखाई।’’
अब वे किसी को क्या बतातीं कि वे बुला ली गयीं, यही क्या कम था ! वैसे उस समारोह में वे तीनों मेल ही कहाँ खा रहे थे ! गाँव-पुरा में वे भले ही मुखिनी बनी रहीं, किन्तु अपनी कोख जाये पुत्र के विवाह में वे लखिया और बिन्दो को समेटे पीछे की कुर्सियों पर दुकी-छिपी अजनबी-सी बैठी रही थीं। समधी के पूछने पर छोटा उन्हें बुला ले गया था तो वे सहमती-सिकुड़ती विशाल स्टेज तक पहुँची थीं—बहू-लड़के ने जग-रीति निभाने को पाँवों का स्पर्श किया तो वे अन्तर्मन तक भीग उठी थीं अपनी ही आर्द्रता से। उसी भावातिरेक में डबडबाई आँखों सहित मुख को बड़े को कानों तक ले गयी थीं—‘‘चाचा-चाची हू बैठे हैं उनके हू....’’वाक्य पूरा नहीं कर पायी थीं कि दुल्हा बने बेटे ने मुख दूसरी ओर फेर लिया तथा किसी नवागन्तुक की बधाई लेने में मशगूल हो गया। परन्तु उन्होंने अपने समधी के नव-जामाता को अनाथ होने के कलुष से तो बचा लिया था और कुछ समय तक वहीं अवांछित-सी खड़ी रहकर पुनः अपनी तीन की बिरादरी में आ मिली थीं। कैसी विकट वेदना महसूस की थी—नौ महीने गर्भ में रखा उन्होंने, पाल-पोसकर खड़ा कर दिया बिन्दो ने और खून-पसीने से सींचता रहा लखिया। मन में असंख्य कीकर-बबूलों की अव्यक्त चुभन लिए अनायास ही दुरियाये से वे तीनों तटस्थ भाव से तमाशाई बने बे-बात सारी रात जागते ब्याह देखते रहे थे।
बस, यही पुनरावृत्ति होती रही हर ब्याह में हर नई बहू के आगमन पर...इसी पीड़ादायिनी स्थिति से गुजरती हुई वे खून को सफेद होते देखती रहीं, हलक में विष उतारती रहीं। खैर, जो भी हुआ, होकर गुजर गया, वे रह तो रही थीं अपने गाँव में, अपने पति के निज आँगन में, बेटों और उनकी गृहस्वामिनी बहुओं से उनका सरोकार ही कितना था ! आँख-ओझल होने का सुख भी कितना बड़ा होता है, उन्होंने यह पहली बार जाना था।
बरस-साल गुजरने लगे लेकिन अचानक एक दिन वह क्षण आया जब गाँव आकर उनके बेटों ने अप्रत्याशित ज्वालामुखी का विस्फोट किया था। और निकलने वाले लावे की झुलस वे आज तक झेल रही हैं आँखें मीचकर...काश, उस दिन उस ज्वालामुखी की आग से वे जलकर भस्म हो गयी होतीं तो बेहतर था।
वे उठना चाहती थीं, पर उठते समय लग रहा था जैसे हाथ-पाँवों का अंश खिंच गया है—अब इतना जाघर कहाँ था कि झमककर उठ पड़ें। कोई उमंग उछाह हो तो बूढ़े हाथ-पाँव भी त्वरित गति से चलने लगते हैं, मन में हील-हुलस ही नहीं तो तन भी शिथिल हो जाता है। जाने के नाम से उन्हें झुरझुरी चढ़ने लगी थी और शरीर में ठीक बुखार के पहले की-सी टूटन। सामान तो रखना ही था, वे बेबस सी उठ खड़ी हुईं। अलगनी पर टँगे अपने कपड़े बटोर लाईं पर उन्हें तहाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, कमरे में पड़ी खाट पर तन ढीला छोड़ बेदम-सी बैठ गईं। लग रहा था माथे के भीतर चक्रवात उठ रहे हैं और कानों में सनसनाहट। कुछ देर बाद खिड़की से बाहर झाँकने की शक्ति बटोर वे खिड़की पर खड़े हो पुकारने लगीं—
‘‘नीटूऽऽऽ अरी नीटूऽऽऊ !’’
‘‘हाँ अम्मा !’’ छोटी पौत्री ने अपने खेल में व्यवधान डाले बिना ही उत्तर दिया।
‘‘अरी यहाँ आ री मेरे झौरें !’’ वे बुलाने लगीं।
लेकिन नीटू नहीं आई, वहीं कंधे उचकाकर रह गई। वे एक-दो बार और आवाज देती रहीं लेकिन नहीं—नीटू नहीं आई। वे खिसियायी-सी अपने कपड़ों को तह करने लगीं। दवा निकालकर रख ली, उसी के लिए पानी माँगना चाहती थीं, लेकिन....मग्धड़ छोकरी।’ वे बुदबुदा उठीं। फिर स्वयं ही जाने को तत्पर हुईं कि बहू गिलास में पानी लेकर हाजिर हो गई। जब यहाँ से जाने का वक्त समीप आता जाता तो बहू अति आर्द्र हो उठती, यह बात वे जानती हैं। दो-चार रोज बहू बड़ी मुस्तैदी से उनकी आज्ञा का पालन करती है, चीजें पल-छिन में हाजिर कर देती है। पर नीटू अभी कहाँ जानती है कि कब अपने व्यवहार में फेर-बदल कर देनी चाहिए ! कभी-कभी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होने लगता है कि इतनी अवस्था जी लेने के बाद भी वे वह सब क्यों नहीं सीख पाईं जो कल की छोकरी इन बहुओं ने गुन लिया। वे कैसी नारियल-सी बनी रहीं, ऊपर से चिकनाई मलना उन्हें जिन्दगी-भर क्यों नहीं आ पाया ?
‘‘अम्मा जी, बाँधि लियौ सामान ?’’ इस घर का नौकर लल्लू पूछ रहा था।
‘‘आजु राति कूँ ही जानौ है, जरूली भइया ?’’ वे अनुनय-सी करती पूछने लगीं कि शायद उनका जाना कुछ दिन और टल जाय।
‘‘देखि लेउ, फिर मेरी फुस्सित नाँय। टैम तो तुम्हारौ हू पूरौ है गयो यहाँ।’’ लल्लू अपनी मजबूरी जताते हुए यहाँ के अनुबन्ध की याद दिलाने लगा।
जाना तो पड़ेगा ही—वे सोचने लगीं और अटैची में हाथ से तहायी दो-चार धोती, ब्लाउज, पेटीकोट निरपेक्ष भाव से डालने लगीं। पर क्या करें, मन बार-बार हिलककर रह जाता वाक्यों की डोर से—
‘‘अम्मा, लखिया आबैगो। कचहरी में तारीख है, सो अम्मा, चाहें दुबक कें ही सही, तुमते मिलि कें जरूल जायगो।’’ गाँव से आया नाई उनसे कह गया था।
पर अभी लखिया की दी हुई तारीख में तो आठ दिन बाकी थे, इतना कौन रुकने देता उन्हें यहाँ। वैसे लखिया से मिलने का जतन तो उन्होंने खोज लिया था। चौराहे से दायें हाथ को जाने वाली गली का मंदिर भी बता दिया था नाई को, कि वे लखिया को उस मंदिर में मिल जाएँगी, पर अब कैसे...? मन में अटूट बेचैनी समेटे वे बहुत देर तक चुप्प अडोल-सी खाट पर बैठी रहीं।
छोटी बहू जल्दी-जल्दी खाना बना रही थी उनके साथ रखने के लिए। ‘‘रेलगाड़ी का खाना अम्मा कैसे पचा पाएँगी, सो जो उन्हें पसन्द है वही बना दिया है, कम-से-कम खा-पीकर तो पहुँचेंगी उनके घर।’’ बहू-बेटे की बतलावन वे साफ सुन रही थीं। इस बहू में कुछ सीमा तक तो सौहार्द्रता है। दिल्ली वाली बहुएँ तो कुछ ज्यादा ही तिनख हैं, वे उनकी बूढ़ी ठूठ काया की सामर्थ्य-असामर्थ्य नहीं पहचानना चाहतीं। तभी न उस दिन बड़ी बहू ने हुक्म सुना दिया था—
‘‘अम्मा जी, आज तो बच्चे चायनीज खाने की जिद कर रहे थे सो उसी में से आया आपको भी दे देगी, खा लेना।’’कहकर बहू पर्स झुलाती हुई घर से बाहर निकल गई। कैसे-कैसे खा पाई थीं उस अजब से भरछत भोजन को। नोन-मिर्च कि सिवई तो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं। इतने बड़े जीवन में सिवइयों को उन्होंने हमेशा घी-बूरे के साथ परोसा था। नूडल्स पेट में डाल तो लिये लेकिन खाते ही पेट फुँक गया था। सिरका और मिर्च के जोड़ ने बूढ़ी आँतों को जला डाला था। अगले दो दिन तक मरोड़ और दस्तों से पीड़ित रही थीं। दोनों बहुएँ फुसफुसा उठी थीं—‘‘देखती नहीं कितना पचा पाएँगी, बस खाए सिद्ध।’’
स्टेशन छोड़ने बेटा-बहू दोनों आए थे। वे चलते समय नीटू और बबली के हाथ पर पाँच-पाँच रुपये रख आई थीं, बहू उन्हें ही लौटा रही थी—‘‘अम्मा जी, आप ही रख लो, आपके काम आएँगे, बच्चों को क्या कमी है।’’
‘‘अरी बच्चन के हाथ पर धर दीजो।’’ कहकर वे मन में कहीं उमेठ महसूस करने लगीं...अकथनीय पीड़ा से अन्दर ही अन्दर तिलमिलाकर रह गईं।
ट्रेन सीटी दे चुकी थी। लल्लू उनकी अटैची और नाश्तेदान थामे उन्हीं के पास आ बैठा था हमेशा की तरह। बेटे ने पैर छुए, उसके बाद बहू ने—‘‘बेटा होय...खाने अघाने रहौ....’’ आशीष देकर वे एक पल को अनचाहे ही आनन्दित हो उठी थीं सब कुछ भूलकर। फिर मन भारी हो उठा, आँखें भर आईं थीं। लेकिन उनसे छुटकारा पाने की जो अतिरिक्त उत्फुल्लता बहू के मुख पर चमक रही थी उसे देख वे अपनी अवांछनीयता पर संतप्त हो उठीं। वे रोना नहीं चाहती थीं फिर भी आँसू आँखों में छितराकर एक धुन्ध-सी छोड़ गए दृष्टि के सामने।
गाड़ी सरक ली थी और शहर से दूर होते उन्हें लग रहा था जैसे वे बेगानेपन के बियाबान में भागती हुई अनन्त रेगिस्तान की ओर जा रही हैं। जहाँ कोई अपना था न आत्मीय....।
‘‘लखिया आवैगो पर लौट जाइगो कम्बखत, ‘वे अपने-आप में ही बुदबुदा रही थीं। अपनी पराश्रिता पर क्रोधित थीं वे। बेटों के कहने से क्यों गाँव छोड़ा ? क्यों अपनी देहरी का मोह तज ममता की मृग-मारीचिका के पीछे भाग लीं, या डर गई थीं वे ? फिर क्यों नहीं दृढ़ होकर खड़ी हो सकी थीं बेटों के समक्ष ? यह वे स्वयं नहीं आज तक जान पायीं। ममता, भय और रक्त का आपसी मेल-जोल खींच लाया था उन्हें यहाँ। अपने मनोबल की कमी पर तब से अब तक पछताती रही हैं। लखिया तो पैरों से लिपटा कैसा हिलककर रोया था—‘‘भाभीऽऽऽई, तू मत जाऽऽय भाभीऽऽऽई...।’’
क्या उत्तर देतीं इस बेजार हूक का, बैलगाड़ी में बैठी सिसकती रही थीं। सिर का पल्ला नीचे सरका लिया था। आधे घूँघट में ही बूढ़ी आँखें बरसती रही थीं, बेटों की सोच का क्या भरोसा ? कलेजे में उठी सुबकी गले में ही घुँटती रही थीं।
वे जिस द्वार-चौखट को छोड़े जा रही थीं, उस घर में सास मरने के कुछ दिन बाद ही ब्याह के आ गई थीं और नववधू का जामा उतार ठेठ घरनी बनी गृहस्थी के उस कठिन प्रश्न-पत्र को हल करने में लग गईं जिसे उनकी सास अधूरा छोड़ गई थीं। जैसी आकांक्षा—वैसा ही परिणाम....वे सास से चार हाथ आगे ही निकली थीं। गृहस्वामिनी के अभाव में जो घर करब के झुये-सा बिखरा जा रहा था उसे उन्होंने तुरन्त बाँहों में भरकर प्रेम-रज्जु से कसकर बाँध दिया था।
वे पखेरुओं के कलरव से पहले उठ जातीं। घर बाहर की झाड़ू-बुहारी, पानी-लत्ता और लीपा-पोती से लेकर ढोर-डंगरों की सानी-पानी सब कर डालतीं। ससुर के लिए दातुन और पानी से भरा सोने-सा दिपदिपाता जगन्नाथी लोटा मोरी पर धर देतीं, झटककर लखिया को जगा लातीं—‘‘सूरज मूड़ पै चढ़ौ है और तुम खटिया पर परे सोइ रहे। उठौ, कुल्ला-दातुन करौ।’’
लखिया कैसा अल्हड़ बछेड़ा-सा मिला था उन्हें, इधर-उधर उजबक-सा फिरता, पाँवों पर ओक बहाए। आँखों में कीचड़ और दाँतों पर पीलेपन की परत....। कुछ दिन तो लिहाज में चुप ही रही थीं—उम्र में छोटा है तो क्या—है तो देवर ही। पर उसकी बावरी वेश-भूषा और गंदेलापन वे ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाई थीं। प्यार से कहतीं तो वह सुनता ही कहाँ था, ज्यादा-से-ज्यादा धुली कमीज पहनकर सिर पर टोपी धर लेता पर टाँगों में वही पट्टे का घुटन्ना लटकाए पूरे गाँव में चकफेरी करता रहता, गिल्ली डंडा बजाता रहता। बड़ी मुश्किल से पाजामा पहनने की आदत डाली थी और कंच्चे-गुच्ची से छुड़ाकर तख्ती पकड़ाकर स्कूल को ठेला था, पर क्या वह तख्ती से आगे बढ़कर स्याही-कापी पकड़ पाया ? तख्ती-टाट पकड़े ही ओठों पर रेख निकल आई थी। हाँ, भाभी के वचन पालन करते-करते जरूर वह पालतू मेमने-सा हो उठा था।
घर में ससुर, विधुर चचिया ससुर, अनब्याहा जेठ, पति, लखिया और मेहनती मजदूरों की रेल-पेल—अच्छा-खासा कुनबा था और अकेली औरत जात—वे। रोटी सेंकने बैठतीं तो सुबह से दोपहर हो आती, पर वे जरा-सी भी तो नहीं डगमगाती थीं कभी। उनकी सहजता देखकर क्या लगता था वे अपनी परिवार की नाजोंपली सबसे छोटी पुत्री होंगी, जिन्हें माँ और भाभियों ने तवे पर चँदिया नहीं डालने दी थी।
उनकी दक्षता देखकर ही तो ससुर ने कनस्तरी-भरे स्वर्ण-आभूषण उन्हें ऐसे सौंप दिए थे जैसे किसी विवाह-गृह से आया लड्डू-कचौड़ी का पड़ोसा हो, और वे उसे कभी उपलों में दाब आतीं, कभी अनाज-भरे गड्डे में गाड़ आतीं। तब बैंकों में रखने का चलन ही कहाँ था—सोचकर अपनी चतुराई पर वे स्वयं ही मुस्कुरा उठीं।
चतुर सुघड़ बहू सम्मान और सराहना की दावेदार थी। कारज-ब्यौहार, परव-त्योहार सबकी अग्रणी बनी रही थीं। समय कैसे सरग के पाखी-सा उड़ा गया, उन्हें खबर ही कहाँ लगी थी, वे तो भोर से साँझ और साँझ से भोर को जीवंत करती रहीं। इसी बीच वे तीन बेटों की माँ बन गईं। लखिया का ब्याह हो गया। लखिया का सम्बन्ध करते समय ससुर जी को उन्होंने कितना रोका था, पड़ौसी का लड़का बुलाकर उससे नाहीं करायी थी, तर्क दिलवाए थे कि लखिया को अभी शादी-ब्याह का क्या शऊर...। लेकिन—
‘‘अब का कल्ला फूटिंगे जा लखिया में,’’ कहते हुए ससुर जी हुक्का गुड़गुड़ाते चौपाल पर निकल गए थे।
जवान-जहान बहू घर पर आ गई तो लखिया कैसा दुबका-दुबका फिरा था। भाभी का पल्ला एक पल को नहीं छोड़ता था। हर काम तो उसने भाभी से पूछकर किया था, फिर अब कैसे...? उसकी भाभी-भक्ति देखकर कभी-कभी तो उन्हें ही खटका होने लगता—बहू क्या सोचेगी....? भाभी का चाकर उसका पति...कैसे बर्दाश्त करेगी ?
धकिया-पिछियाकर किसी तरह रात को बहू के पास भेजा था, पर वहाँ भी ढाक के तीन पात !
वे सवेरे ही बहू के पास जाना चाह रही थीं पर बार-बार हिम्मत बाँधने पर भी मन अड़ियल तुरंग-सा पीछे हटता ही चला जाता—कैसे पूछेंगी नई ब्याही से कि इस लखिया में मरदपने के लच्छन हैं कि नहीं ? वयस में वे बहू की कोई हमउम्र तो थीं नहीं। लेकिन चिन्ता रात-भर उन्हें दीमक-सा खाती रही थी, एक पल को पलक नहीं मूँद सकी थीं...उसी बेचैनीवश पूछ बैठी थीं रात की बात...। बहू खिलखिलाकर हँस पड़ी थी।
‘‘काहे को हँस रही है री बिन्दो....बता न !’’ वे स्वयं नई दुल्हन की तरह शरमा उठी थीं, नीची आँखें किए कपोलों पर लाली दौड़ गई थी।
‘‘जीजीऽऽई...जीजीऽऽ हऽहऽहऽहऽअ !’’ बिन्दो हँसी नहीं रोक पा रही थी।
‘‘अब कछु बोलैगी हू कै हसति ही रहेगी,’’ वे आतुरता से भर उठी थीं—‘‘बोल जल्दी।’’
‘‘जीजी, हऽऽअ हऽऽ ! जीजी, काहे को भेजि दीये तुमने ? पहले तो नीचे कू मुँह करें ठाड़े ही रहे, फिर हाल भये पिल्ला से कुँइ-कुँइ करि कें सोई गए। मैं झकझोरि-झकझोरि कें हारि गयी, अब तक नाहिं उठे। अब तुम हि जगाय लेउ जाय कें !’’
उन्होंने अपने माथे पर हाथ दे मारा—‘‘हाय मेरे राम जी !’’ वे क्या कहती बिन्दो से कि यह हौलू बिल्लाल निरा औघड़ है। अरे, खाना-पीना और यह सब...तो चिरई-चिरवा भी जानते हैं, फिर यह तो मानस-मनिख का पूतरा, कौन समझाए इस मूरख को ! वे अजीब-सी दुविधामयी चिन्ता से घिर उठी थीं। वह तो बिन्दो समझदार निकली कि बालक की तरह भाभी के पल्लू से बँधे पति के प्रति कभी रोष प्रकट नहीं किया।
सारे घर का काम उठा लिया था बिन्दो ने। अपनी जीजी को तो किसी काम से हाथ नहीं लगाने देती। लेना-देना, ऊपर का इन्तजाम और घर की मुख्तारी ही रह गई थी उनके जिम्मे। जिठानी के तीनों बच्चों का लालन-पालन भी बिन्दो ने अपनी ही गोद में डाल लिया था। वे पूजा करते-करते सौ-सौ बार ठाकुरजी को माथा झुकातीं कि हे मेर पिरभू ! लखिया के बचपन को हाथ लगाकर जरा-सा सगुना क्या दिया, मुझे बदले में ऐसी हिरदय की टूक सहोदरा बख्श दी !
मजाल है कि बिन्दो जीजी के बिना कौर तोड़ जाय। वे हजार बार कहतीं—‘‘अरी बिन्दो, खाय लै री ! कब तक भूखी बैठी रहैगी ?’’ पर वह दोनों का भोजन एक ही थाली में परोसकर बैठ जाती—‘‘आ जाऔ जीजी, अब बहौत है गयी पूजा। और कहा माँगि रही हौ राम जी पै। सब तौ है।’’ कहकर जोर से हँसने लगती। बिन्दो हरगिज ग्रास न तोड़ती जब तक कि वे तुलसी के चौरा पर लौटा न ढार लेतीं।
बहुत समय बीत गया था पर बिन्दो के गर्भ में आस नहीं ठहरी थी। मुहल्ले में खुसुर-पुसुर होने लगी थी। वे घबरा उठी थीं बहुत अधिक।
जब पहले-पहले बिन्दो के पाँव भारी हुए तो उन्हें लगा था वे ताई नहीं, दादी बनने जा रही हैं। हौंस-हुलस से भरी वे कृष्ण कन्हैया और यशोदा के गीत गाया करतीं। हाथोंहाथ रखतीं बिन्दो को; पर वह भी मरी बड़ी अड़ियल थी, न जाने कब खेत पर जाकर चौड़ी नाली का पाट फलाँग गयी। तबीयत बिगड़ी तो वे बैलगाड़ी में धरे इस डॉक्टर से उस डॉक्टर पर भागती रही थीं लेकिन कहाँ ठीक हो सका था...कच्चा ही गिर गया, बिन्दो ही बड़ी मुश्किल से बच पायी थी।
उनके पति को न जाने कौन-सा रोग लगा था कि गँवई-गाँव से लेकर शहर तक के इलाज़-उपचार हुए लेकिन वे एक दिन....और इसी तरह ससुर, चचिया ससुर मृत्यु-पथ पर अनुगामी बने चल दिए। अनब्याहे जेठ तो कब के साधू होकर चले गए थे। बड़ों का साया सिर से उठ गया। रह गए वे और लखिया, अनाथ हुए पूरी गृहस्थी का वजन लिए। पर लखिया समय का नाजुक मिजाज पहचानकर रातोंरात कैसे घर का पालनहार बनकर खड़ा हो गया कि वे स्वयं विस्मित रह गयी थीं। उनके तीनों बच्चों की पढ़ाई में रंचमात्र का अंतर नहीं आने दिया लखिया ने। भीषण लू-लपट और शीत सरकती रातों को बराबर करके वह बैलों के साथ बैल की नाईं जुतता रहता। रक्त-स्वेद मिलाकर धरती की कोख में बीज बोता रहा और फसल समेट-बेचकर भाभी के हाथ पर पाई-पाई रखता रहा। भतीजों को पढ़ा-लिखाकर योग्य बनाने का व्रत साध वह स्वयं धरती की धूल में मिलता रहा था।
आड़ा समय भी निकल गया अच्छे ही वक्त की तरह। तीनों बेटे बड़े हो गए। बड़े दोनों दिल्ली में नौकरी करने लगे, छोटा आगरा बैंक में मैनेजर हो गया। लखिया का श्रम सफल हो गया था। वे निछावर हो गयी थीं पुत्र-सरीखे देवर पर। शादी की बात आयी तो जाहिर है कितने ही धनाढ्य शहरी कन्याओंके पिता उनके बेटों के ससुर बनने का सौभाग्य खोजने लगे। उन पिताओं को योग्य दामाद चाहिए थे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं...। शादी भी उनके बेटों ने शहर में पली-पुसी कन्याओं से की, गाँव की अल्हड़ गँवार को वे कैसे निभा पाते ! शादी की बाबत बेटे ने माँ और चाचा को पूछा ही कहाँ ही था, बस खबर दे दी थी कि इस-इस तारीख को चले आयें, सो वे लखिया और बिन्दो को लेकर चली गयी थीं। गाँव आकर बड़े ताने-उलाहने सुनने पड़े थे—‘‘बेटा ब्याहि लियौ और एक खीकरी तक न दिखाई।’’
अब वे किसी को क्या बतातीं कि वे बुला ली गयीं, यही क्या कम था ! वैसे उस समारोह में वे तीनों मेल ही कहाँ खा रहे थे ! गाँव-पुरा में वे भले ही मुखिनी बनी रहीं, किन्तु अपनी कोख जाये पुत्र के विवाह में वे लखिया और बिन्दो को समेटे पीछे की कुर्सियों पर दुकी-छिपी अजनबी-सी बैठी रही थीं। समधी के पूछने पर छोटा उन्हें बुला ले गया था तो वे सहमती-सिकुड़ती विशाल स्टेज तक पहुँची थीं—बहू-लड़के ने जग-रीति निभाने को पाँवों का स्पर्श किया तो वे अन्तर्मन तक भीग उठी थीं अपनी ही आर्द्रता से। उसी भावातिरेक में डबडबाई आँखों सहित मुख को बड़े को कानों तक ले गयी थीं—‘‘चाचा-चाची हू बैठे हैं उनके हू....’’वाक्य पूरा नहीं कर पायी थीं कि दुल्हा बने बेटे ने मुख दूसरी ओर फेर लिया तथा किसी नवागन्तुक की बधाई लेने में मशगूल हो गया। परन्तु उन्होंने अपने समधी के नव-जामाता को अनाथ होने के कलुष से तो बचा लिया था और कुछ समय तक वहीं अवांछित-सी खड़ी रहकर पुनः अपनी तीन की बिरादरी में आ मिली थीं। कैसी विकट वेदना महसूस की थी—नौ महीने गर्भ में रखा उन्होंने, पाल-पोसकर खड़ा कर दिया बिन्दो ने और खून-पसीने से सींचता रहा लखिया। मन में असंख्य कीकर-बबूलों की अव्यक्त चुभन लिए अनायास ही दुरियाये से वे तीनों तटस्थ भाव से तमाशाई बने बे-बात सारी रात जागते ब्याह देखते रहे थे।
बस, यही पुनरावृत्ति होती रही हर ब्याह में हर नई बहू के आगमन पर...इसी पीड़ादायिनी स्थिति से गुजरती हुई वे खून को सफेद होते देखती रहीं, हलक में विष उतारती रहीं। खैर, जो भी हुआ, होकर गुजर गया, वे रह तो रही थीं अपने गाँव में, अपने पति के निज आँगन में, बेटों और उनकी गृहस्वामिनी बहुओं से उनका सरोकार ही कितना था ! आँख-ओझल होने का सुख भी कितना बड़ा होता है, उन्होंने यह पहली बार जाना था।
बरस-साल गुजरने लगे लेकिन अचानक एक दिन वह क्षण आया जब गाँव आकर उनके बेटों ने अप्रत्याशित ज्वालामुखी का विस्फोट किया था। और निकलने वाले लावे की झुलस वे आज तक झेल रही हैं आँखें मीचकर...काश, उस दिन उस ज्वालामुखी की आग से वे जलकर भस्म हो गयी होतीं तो बेहतर था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book