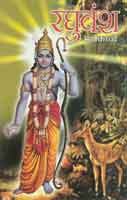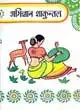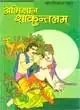|
धर्म एवं दर्शन >> रघुवंश महाकाव्य रघुवंश महाकाव्यकालिदास
|
16 पाठक हैं |
||||||
रघुवंश महाकाव्य का हिन्दी भावानुवाद...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
महाकवि कालिदास हमारे राष्ट्रीय कवि थे। वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के
प्रतीक थे। इस विशाल तथा विराट देश की संस्कृति कालिदास की वाणी में बोलती
है अंग्रेजों के आगमन के समय वह भारत वर्ष संसार की दृष्टि में
संस्कृतिविहीन व अंधकारपूर्ण देश समझा जाता था, परन्तु कालिदास की कृतियों
ने ही भारत के प्रति विश्व का आदर-भाव जगाने का प्रशंसनीय कार्य किया।
रघुवंश जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हैं, इसमें रघु के कुल में उत्पन्न राजाओं का वर्णन किया गया है। इसमें राजा दिलीप, रघु, दशरथ,राम,कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। वे सभी राजा समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए। प्रभुश्री राम का रघुवंश महाकाव्य में विशेष रूप से वर्णन किया गया है।
रघुवंश जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हैं, इसमें रघु के कुल में उत्पन्न राजाओं का वर्णन किया गया है। इसमें राजा दिलीप, रघु, दशरथ,राम,कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। वे सभी राजा समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए। प्रभुश्री राम का रघुवंश महाकाव्य में विशेष रूप से वर्णन किया गया है।
रघुवंश महाकाव्य
कालिदास की कृतियों के क्रम में रघुवंश महाकाव्य का तीसरा स्थान है। प्रथम
दो कृतियां हैं- कुमारसंभव और मेघदूत।
कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे निपट मूर्ख और उजड्ड थे। फिर वे इतने विद्वान और ऐसी अनन्य कृतियों के रचयिता किसी प्रकार बन गए। इस विषय में एक किंवदंति प्रचलित है। उसका सार संक्षेप यही है कि कुछ विद्वानों ने विदुषी विद्योत्तमा की विद्वता से चिढ़कर षड्यंत्र रचा और निपट मूर्ख कालिदास से उसका विवाह करा दिया। विदुषी विद्योत्तमा को जब कालिदास की वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उसने उसके लिए अपने घर के द्वार बंद कर दिए। कालिदास मर्माहत से घर से निकल पड़े और उन्होंने साधना करके विद्यार्जन किया और जब विद्वान बन घर लौटे तो उपने द्वार पर दस्तक दी और कालिदास ने कपाट खटखटाते हुए कहा- द्वारं देहि अनावृत्तं कपाटम् जब यह स्वर विद्योत्तमा को सुनाई दिया तो उसने पूछा ‘अस्ति कश्चिद् वाग् विशेषः।’ अर्थात कौन है, ऐसी उत्कृष्ठ वाणी का विशेषज्ञ ?’
यह प्रचलित है कि अपनी पत्नी के प्रथम वाक्य के तीन शब्दों को लेकर उन्होंने तीन वाक्यों की रचना कर डाली। ‘अस्ति’ शब्द से कुमारसंभव का प्रथम श्लोक ‘कश्चिद्’ से मेघदूत का प्रथम श्लोक और ‘वाक्’ से रघुवंश का प्रथम श्लोक आरंभ किया।
यहां हम केवल रघुवंश की बात कर रहे हैं-
रघुवंश काव्य के आरंभ में महाकवि ने रघुकुल के राजाओं का महत्त्व एवं उनकी योग्यता का वर्णन करने के बहाने प्राणिमात्र के लिए कितने ही प्रकार के रमणीय उपदेश दिये हैं। जिस कार्य को कोई बड़े से बड़ा सुधारक चारों ओर घूमकर उपदेश की झड़ी लगा करके कर सकता है, उसे कवि संसार के एक कोने में बैठा हुआ अपनी लेखनी के बल से सदा के लिए कर दिखाता है।
रघुवंश काव्य में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं को निमित्त बनाकर उदारचरित पुरुषों का स्वभाव पाठकों के सम्मुख रखा है। रघुवंशी राजाओं का संक्षेप में वर्णन जानना हो तो रघुवंश के केवल एक श्लोक में उसकी परिणति इस प्रकार है-
कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे निपट मूर्ख और उजड्ड थे। फिर वे इतने विद्वान और ऐसी अनन्य कृतियों के रचयिता किसी प्रकार बन गए। इस विषय में एक किंवदंति प्रचलित है। उसका सार संक्षेप यही है कि कुछ विद्वानों ने विदुषी विद्योत्तमा की विद्वता से चिढ़कर षड्यंत्र रचा और निपट मूर्ख कालिदास से उसका विवाह करा दिया। विदुषी विद्योत्तमा को जब कालिदास की वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उसने उसके लिए अपने घर के द्वार बंद कर दिए। कालिदास मर्माहत से घर से निकल पड़े और उन्होंने साधना करके विद्यार्जन किया और जब विद्वान बन घर लौटे तो उपने द्वार पर दस्तक दी और कालिदास ने कपाट खटखटाते हुए कहा- द्वारं देहि अनावृत्तं कपाटम् जब यह स्वर विद्योत्तमा को सुनाई दिया तो उसने पूछा ‘अस्ति कश्चिद् वाग् विशेषः।’ अर्थात कौन है, ऐसी उत्कृष्ठ वाणी का विशेषज्ञ ?’
यह प्रचलित है कि अपनी पत्नी के प्रथम वाक्य के तीन शब्दों को लेकर उन्होंने तीन वाक्यों की रचना कर डाली। ‘अस्ति’ शब्द से कुमारसंभव का प्रथम श्लोक ‘कश्चिद्’ से मेघदूत का प्रथम श्लोक और ‘वाक्’ से रघुवंश का प्रथम श्लोक आरंभ किया।
यहां हम केवल रघुवंश की बात कर रहे हैं-
रघुवंश काव्य के आरंभ में महाकवि ने रघुकुल के राजाओं का महत्त्व एवं उनकी योग्यता का वर्णन करने के बहाने प्राणिमात्र के लिए कितने ही प्रकार के रमणीय उपदेश दिये हैं। जिस कार्य को कोई बड़े से बड़ा सुधारक चारों ओर घूमकर उपदेश की झड़ी लगा करके कर सकता है, उसे कवि संसार के एक कोने में बैठा हुआ अपनी लेखनी के बल से सदा के लिए कर दिखाता है।
रघुवंश काव्य में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं को निमित्त बनाकर उदारचरित पुरुषों का स्वभाव पाठकों के सम्मुख रखा है। रघुवंशी राजाओं का संक्षेप में वर्णन जानना हो तो रघुवंश के केवल एक श्लोक में उसकी परिणति इस प्रकार है-
शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्।
वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनानन्ते तनुत्यजाम्।।
वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनानन्ते तनुत्यजाम्।।
अर्थात- बाल्यकाल में विद्याध्यन करते थे,
यौवन में
सांसारिक भोग भोगते थे, बुढ़ापे में मुनियों के सामने रहते थे और अन्त में
योग के द्वारा शरीर छोड़ते थे।
किंतु उनके इस कथन में अंत में एक विरोधाभाष आ गया है। रघुवंश महाकाव्य के अंत में कालिदास ने अग्निवर्ण का वर्णन किया है, जो कि पतित होकर क्षयग्रस्त हो गया था और उसी से उसका प्राणांत भी हुआ। किंतु इसके लिए कालिदास का स्पष्टीकरण है कि अग्निवर्ण के पिता सुदर्शन अपने राज्य की इस प्रकार सुंदर व्यवस्था कर गए थे कि अग्निवर्ण को करने के लिए कुछ रहा ही नहीं तो उसमें कामनाओं और वासनाओं की प्रबलता होने लगी और वह पतन के गर्त में गिरता चला गया।
अग्निवर्ण के मरणोपरांत उसकी गर्भवती पत्नी के राज्यभिषेक के उपरांत इस महा काव्य की इतिश्री होती है। कालिदास ने इस महाकाव्य का ऐसा अंत क्यों किया ? इस विषय पर विद्वानों की लेखनी मौन है। तदपि इससे रघुवंश का महत्व कम नहीं हो जाता। जिस कुल में आद्योपांत आदर्श पुत्र ही जन्म लेते रहे, कालांतर में यदि उस कुल में एक ऐसा आदर्शहीन उत्पन्न हो भी गया तो वह नगण्य है। सूर्यवंशी राजाओं और क्षत्रियों को आज भी सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाता है।
‘रघुवंश’ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसमें रघु के कुल में उत्पन्न राजाओं का वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश, और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। वे सभी समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए।
राम का इसमें विषद वर्णन किया गया है। उन्नीस में से छः सर्ग उनसे ही संबंधित हैं।
महाकवि कालिदास हमारे राष्ट्रीय कवि थे। वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक थे। इस विशाल तथा विराट देश की संस्कृति कालिदास की वाणी में बोलती है। अंग्रेजों के आगमन के समय यह भारतवर्ष संसार की दृष्टि में संस्कृति विहीन अंधकारपूर्ण देश समझा जाता था। परंतु कालिदास की कृतियों ने ही भारत के प्रति विश्व का आदर जगाने का श्लाघनीय कार्य किया।
कालिदास का उपदेश है-
‘इस जीवन को महान लाभ मानना चाहिए तथा इसे सफल बनाने के लिए धर्म, अर्थ तथा काम का सामंजस्य प्रस्तुत करना चाहिए।’
इसी प्रकार की भावना उनके सभी ग्रन्थों में पाई जाती है।
डायमंड पाकेट बुक्स के श्री नरेन्द्रकुमार की रूझान प्राचीन साहित्य की ओर बहुत पहले से है और उन्होंने निश्चय किया है कि वे कालिदास की सभी कृतियों का हिन्दी रूपांतरण अपने पाठकों के लाभार्थ हेतु प्रस्तुत करेंगे। उस प्रयास में इससे पूर्व ‘अभिज्ञान-शाकुंतलम्’ पाठकों के हाथ में आ चुकी है. यह दूसरी कृति ‘रघुवंश महाकाव्य’ दी जा रही है और भविष्य में इसी प्रकार अन्य सभी कृतियां प्रकाशित होती रहेंगी।
लेखक और प्रकाशक का प्रयास तभी सफल माना जाता है जब पाठक उसे मन से ग्रहण करें। आशा है कि हमारे पाठक इन कृतियों से अवश्य लाभान्वित होंगे।
प्रथम सर्ग
किंतु उनके इस कथन में अंत में एक विरोधाभाष आ गया है। रघुवंश महाकाव्य के अंत में कालिदास ने अग्निवर्ण का वर्णन किया है, जो कि पतित होकर क्षयग्रस्त हो गया था और उसी से उसका प्राणांत भी हुआ। किंतु इसके लिए कालिदास का स्पष्टीकरण है कि अग्निवर्ण के पिता सुदर्शन अपने राज्य की इस प्रकार सुंदर व्यवस्था कर गए थे कि अग्निवर्ण को करने के लिए कुछ रहा ही नहीं तो उसमें कामनाओं और वासनाओं की प्रबलता होने लगी और वह पतन के गर्त में गिरता चला गया।
अग्निवर्ण के मरणोपरांत उसकी गर्भवती पत्नी के राज्यभिषेक के उपरांत इस महा काव्य की इतिश्री होती है। कालिदास ने इस महाकाव्य का ऐसा अंत क्यों किया ? इस विषय पर विद्वानों की लेखनी मौन है। तदपि इससे रघुवंश का महत्व कम नहीं हो जाता। जिस कुल में आद्योपांत आदर्श पुत्र ही जन्म लेते रहे, कालांतर में यदि उस कुल में एक ऐसा आदर्शहीन उत्पन्न हो भी गया तो वह नगण्य है। सूर्यवंशी राजाओं और क्षत्रियों को आज भी सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाता है।
‘रघुवंश’ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसमें रघु के कुल में उत्पन्न राजाओं का वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश, और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। वे सभी समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए।
राम का इसमें विषद वर्णन किया गया है। उन्नीस में से छः सर्ग उनसे ही संबंधित हैं।
महाकवि कालिदास हमारे राष्ट्रीय कवि थे। वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक थे। इस विशाल तथा विराट देश की संस्कृति कालिदास की वाणी में बोलती है। अंग्रेजों के आगमन के समय यह भारतवर्ष संसार की दृष्टि में संस्कृति विहीन अंधकारपूर्ण देश समझा जाता था। परंतु कालिदास की कृतियों ने ही भारत के प्रति विश्व का आदर जगाने का श्लाघनीय कार्य किया।
कालिदास का उपदेश है-
‘इस जीवन को महान लाभ मानना चाहिए तथा इसे सफल बनाने के लिए धर्म, अर्थ तथा काम का सामंजस्य प्रस्तुत करना चाहिए।’
इसी प्रकार की भावना उनके सभी ग्रन्थों में पाई जाती है।
डायमंड पाकेट बुक्स के श्री नरेन्द्रकुमार की रूझान प्राचीन साहित्य की ओर बहुत पहले से है और उन्होंने निश्चय किया है कि वे कालिदास की सभी कृतियों का हिन्दी रूपांतरण अपने पाठकों के लाभार्थ हेतु प्रस्तुत करेंगे। उस प्रयास में इससे पूर्व ‘अभिज्ञान-शाकुंतलम्’ पाठकों के हाथ में आ चुकी है. यह दूसरी कृति ‘रघुवंश महाकाव्य’ दी जा रही है और भविष्य में इसी प्रकार अन्य सभी कृतियां प्रकाशित होती रहेंगी।
लेखक और प्रकाशक का प्रयास तभी सफल माना जाता है जब पाठक उसे मन से ग्रहण करें। आशा है कि हमारे पाठक इन कृतियों से अवश्य लाभान्वित होंगे।
-अशोक कौशिक
प्रथम सर्ग
वसिष्ट के आश्रम में
मंगलाचरण-
‘वाणी और अर्थ जैसे अलग कहलाते हुए
भी एक हैं, वैसे
ही पार्वती और शिव कहने के लिए तो दो विभिन्न रूप में हैं परन्तु वास्तव
में वे एक ही हैं, इसीलिए वाणी और अर्थ को ठीक प्रकार से समझने के लिए,
मैं संसार की माता पार्वती जी और पिता शिवजी को प्रणाम करता हूं, वे शिव
और पार्वती शब्द और अर्थ के समान परस्पर मिले हुए हैं अर्थात एक रूप हैं।
रघुओं के वंश का वर्णन-
मैं रघुवंश का वर्णन करने के लिए उद्यत तो हो
रहा हूं
किंतु मुझे लग रहा है कि कहां तो सूर्य के समान तेजस्वी वह वंश, जिस वंश
के आरंभ में ‘रघु’ और कालांतर में राम जैसे
महापराक्रमी धीर,
वीर, उदात्त चरित्र वाले महापुरुष उत्पन्न हुए हैं और कहां बड़ा ही मंद
मति वाला मैं। ऐसे रघुवंश का पार पा सकना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए नितांत
असंभव है, यह मैं भली-भांति जानता हूं, फिर भी मैं साहस करके यह प्रयत्न
कर रहा हूं और इस समय मेरी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कि मानों तिनकों से
बनी छोटी सी नाव को लेकर मैं अपार और गहन सागर को पार करने की बात सोच रहा
हूं।
एक बात और, मैं हूं तो मंदबुद्धि वाला व्यक्ति किंतु मेरी साध यह है कि प्रख्यात कवियों के समान मुझे भी यश प्राप्त हो। लोग यदि मेरे इस साध के विषय में सुनेंगे तो मुझ पर बहुत हंसेंगे। क्योंकि इस संबंध में मेरी स्थिति ठीक उस बौने व्यक्ति के समान है जो दूर ऊंचे पेंड़ पर लगे उन फलों को तोड़ने के लिए साध लिए हो जिनको केवल लंबे व्यक्ति और लंबे हाथ वाले ही पा सकते हैं।
किंतु इसमें भी एक संतोष की बात यह है कि पूर्व काल में महर्षि वाल्मीक आदि महान कवियों ने उनके विषय में सुंदर काव्य लिख करके मेरे लिए वाणी का द्वार खोल दिया है। इसलिए इस विषय की पैठ अब मेरे लिए सरल हो गई है, यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कि मोतियों को पहले ही बांध दिया हो, उसमें फिर सुई से धागा पिरोना बहुत ही सुगम हो जाता है।
जैसा कि मैंने आरंभ में ही कह दिया है कि मैं नितांत मंदमति हूं, मुझे कुछ आता-जाता नहीं। फिर भी मैं उन रघुवंशियों का वर्णन करने के लिए समुद्यत हूं-
जिनके चरित्र जन्म से आरंभ करके अंत तक शुद्ध और पवित्र रहे हैं, जो किसी काम का जब बीड़ा उठाते थे उसको पूर्ण करके ही विराम लेते थे, जो समुद्र के ओर-छोर तक फैली हुई यह धरती है, उसके स्वामी थे और जिनके रथ पृथ्वी से स्वर्ग तक सीधे जाया करते थे।
जो नित्य नियम पूर्वक शास्त्रों की विधि से यज्ञ किया करते थे, जो याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार मुंह-मांगा और मनचाहा दान दिया करते थे, जो अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार ही दंड देते थे और जो अवसर देखकर ही तदनुरूप कार्य किया करते थे।
जो रघुवंशी केवल त्याग के लिए, दान करने के लिए ही धन का संग्रह किया करते थे, और जो सत्य के पालन के लिए बहुत कम बोला करते थे। अभिप्राय यह है कि जितना कहा जाए उसका अक्षरशः पालन किया जाए, जो केवल यश प्राप्ति के लिए ही अन्य देशों को जीतते थे, उन राज्यों को अपने वश में करने अथवा वहां लूटपाट करने के लिए नहीं और जो केवल प्रजा के लिए अर्थात अपनी संतान प्राप्ति के लिए ही गृहस्थ में प्रविष्ट होते थे, भोग विलास के लिए नहीं।
जो बाल्यकाल में सभी को अध्ययन कर उनमें पारंगत होते थे और तरुणाई में संसार के भोगों का आनन्द लेते थे। इसके उपरांत तृतीयावस्था में वनों में जाकर मुनिवृत्ति धारण करते हुए तपस्या करते थे और अंत में ब्रह्म अथवा परमात्मा का ध्यान करते हुए योग द्वारा पार्थिव शरीर को शांत करते थे
इस प्रकार के जो रघुवंशी थे, इन गुणों से संपन्न जो वंश था, उससे ही प्रभावित होकर मैं यह काव्य लिखने के लिए प्रेरित हुआ हूं।
इस काव्य को, अर्थात रघुकुल के इस गुणानुवाद को सुनने के अधिकारी भी वे ही संत सज्जन हो सकते हैं, जिनमें भले-बुरे की परख की योग्यता है।
क्योंकि सोना खरा है अथवा खोटा इसका पता तो तब ही लग सकता है जब उसको अग्नि में तपाया जाए।
अब मैं उस वंश का वर्णन करता हूं-
जिस प्रकार वेद के छंदों में सर्वप्रथम आकार के लिए स्थान है उसी प्रकार राजाओं में सर्वप्रथम सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए हैं। मनु महाराज बड़े मनीषि थे और मनीषियों में बड़े माननीय और आदरणीय माने जाते थे।
उन्हीं वैवस्वत मनु के उज्जवल वंश में चन्द्रमा के समान सबको सुख प्रदान करने वाले और बहुत ही शुद्ध चरित्र वाले राजा दिलीप ने जन्म लिया। उनके जन्म से ऐसा लगा मानों क्षीर सागर में चंद्रमा ने जन्म लिया हो।
राजा दिलीप के शरीर सौष्ठव का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं-
दिलीप का रूप देखने योग्य था उनकी छाती खूब चौड़ी थी। वे वृषस्कंध अर्थात सांड के समान चौड़े कंधों वाले थे, उनकी भुजाएं शाल के वृक्ष के समान लम्बी-लम्बी थीं। उनका अपार तेज देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो क्षत्रियों का जो वीरत्व धर्म है उनके शरीर में यह समझ कर प्रविष्ट हो गया हो कि सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों के संहार करने का जो उसका काम है वह इस शरीर के माध्यम से अवश्य पूर्ण हो सकेगा।
जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता से संसार के सब दृढ़ पदार्थों को दबा लिया है और अपनी चमक से उसने सब चमकीली वस्तुओं की चमक को घटा दिया है, तथा अपनी ऊंचाई से सब ऊंची वस्तुओं को नीचा कर दिया है एवं अपने विस्तार से सारी पृथ्वी को ढक लिया है। ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप ने अपने बल, तेज और सुदृढ़ शरीर से सबको एक प्रकार से विजित-सा करके सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया है।
जैसा उनका सुंदर रूप था ठीक उसी प्रकार उनकी बुद्धि भी थी और जैसी उनकी तीव्र बुद्धि थी उसके अनुसार उन्होंने शीघ्र ही सब शास्त्रों को पढ़ लिया था। इसलिए वे शास्त्रानुसार ही अपना कार्य करते थे इसलिए उनको तदनुरूप ही सफलता भी प्राप्त होती थी।
जिस प्रकार समुद्री भयानक जंतु मगर तथा घड़ियाल आदि के भय से लोग समुद्र में प्रविष्ट होने से डरते हैं, वैसे ही राजा दिलीप के सेवक आदि उनसे डरते थे। उसका मुख्य कारण यह था कि वे न्याय करने में बड़े कठोर थे, वे किसी का पक्षपात नहीं करते थे। किन्तु समुद्र के सुंदर रत्नों की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार लोग समुद्र में प्रविष्ट होते हैं ठीक उसी प्रकार दयालु, उदार, गुणवान, राजा दिलीप की कृपा पाने के लिए उनके सेवक सदा उनका मुख भी जोहते रहते थे।
ज्यों चतुर सारथी जिस प्रकार रथ चलाता है उस समय उसके रथ के पहिए बाल भर भी लीक से बाहर नहीं हो पाते, उस प्रकार राजा दिलीप ने प्रजा की भी ऐसी पालना की कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति मनु द्वारा निर्दिष्ट नियमों से बाल भर भी बाहर नहीं जाता था। सब लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रम में रहते हुए अपने-अपने धर्म का यथावत पालन करते थे।
जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जल शोख कर फिर वर्षा के रूप में उससे अनेक गुणा अधिक उसको ही प्रदान करता है उसी प्रकार राजा दिलीप भी प्रजा से राजस्व प्राप्त करके फिर प्रजा की भलाई में उसको व्यय कर देते थे। प्रजा की भलाई के लिए ही वे प्रजा से ही कर लिया करते थे।
परंपरा के अनुसार जिस प्रकार अन्याय राजाओं के पास बड़ी-बड़ी सेनाएं होती हैं उसी प्रकार राजा दिलीप की यह सेना केवल शोभा के लिए ही थी स्वयं राजा दिलीप जितने शास्त्रों में निष्णात थे। उतने ही वे धनुर्विद्या में भी निपुण थे। इसलिए अपना सारा कार्य वे अपनी चतुर बुद्धि और धनुष पर चढ़ी डोरी से ही निकाल लिया करते थे।
राजा दिलीप न तो किसी को अपने मन का भेद बताते थे और न अपनी भंगिमाओं से अपने मन की बात किसी को जानने देते थे। जैसे किसी व्यक्ति के इस जन्म के जीवन में उसके सुखी अथवा दुखी देखकर लोग यह अनुमान लगाने लगते हैं उसने पिछले जन्म में उसी प्रकार के अच्छे अथवा बुरे कर्म किए होंगे वैसे ही राजा दिलीप के मन की बात भी लोग तभी जान पाते थे जब कि वह किसी कार्य को संपन्न कर लेते थे।
राजा दिलीप निडर होकर अपनी रक्षा करते थे, बड़े धीरज के साथ वे अपने धर्म का पालन करते थे, धन एकत्रित करने में उनको किसी प्रकार का लोभ नहीं सताता थ, लोभ का त्याग करके ही वे धन का संग्रह करते थे, इसी प्रकार के संसार के सुख का भी उनमें किसी प्रकार का मोह नहीं था।
मनुष्य में यदि किसी प्रकार का कोई गुण हुआ तो वह उसका बखान करता फिरता है। वीर वीरता का, दानी अपने दान का, विद्वान अपनी विद्या को आदि आदि, जिससे कि संसार में उसका नाम हो सके। किन्तु राजा दिलीप का स्वभाव ऐसा नहीं था। वे सब कुछ जान कर भी चुप रहते थे अर्थात अपनी विद्वता का ढिढोरा नहीं पीटते थे, शत्रुओं को जहां तक संभव होता था, वे क्षमा कर दिया करते थे, दान देकर भी कभी उन्होंने उसके विषय में बखान नहीं किया। उनके इस प्रकार के निराले व्यवहार को देखकर ऐसा अनुभव होता था कि चुप रहने, क्षमा करने और प्रशंसा से दूर भागने के गुण भी उनमें ज्ञान, शक्ति और त्याग के साथ ही उत्पन्न हुए थे।
राजा दिलीप संसार के भोगों को अपने पास फटकने नहीं देते थे। सारी विद्याओं में वे निष्णात थे। उनका अपना सारा जीवन दिन-रात धर्म में ही लगा रहता था। इस प्रकार छोटी-सी अवस्था में भी वे इतने निपुण और इतने चतुर हो गए थे कि बुढ़ापा आए बिना भी उनकी गणना बूढ़ों में होने लगी थी। अर्थात उनको परिपक्व बुद्धि का प्रौढ़ व्यक्ति माना जाता था।
पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रों को बुरा काम करने से रोके और शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त करे, सब प्रकार से उनका पालन-पोषण और रक्षा करता हुआ उन्हें योग्य बनाए। ठीक उसी प्रकार महाराजा दिलीप भी अपनी प्रजा का पुत्रवत् पालन करते हुए उसका भरण-पोषण करते थे और विपत्ति से उनकी रक्षा करते थे अर्थात सब प्रकार से उनका संरक्षण करते थे। इस प्रकार पिता तो केवल जन्म देने वाले ही थे वास्तव में राजा दिलीप ही सब प्रकार से उसके पिता समान थे।
राजा का धर्म है कि वह अपराधी को दंडित करे, इसके बिना राज्यस्थिर नहीं रहता। इसलिए वे अपराधियों को अवश्य दंड देते थे। संतान उत्पन्न करके वंश चलाने के लिए ही उन्होंने विवाह किया था। भोग विलास के लिए नहीं। इस प्रकार दंड और विवाह यद्यपि अर्थ और काम शास्त्र के विषय है फिर भी राजा के हाथों में पहुंचकर वे धर्म ही बन गए थे।
वे प्रजा से जो कर लिया करते थे उसको वे इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में लगा दिया करते थे। इस प्रकार इन्द्र उनसे प्रसन्न होकर आकाश से उनकी प्रजा पर दृष्टि रखता था, इस प्रकार उनके राज्य में खूब खेती लहलहाती थी। राजा दिलीप और इंद्र एक दूसरे को प्रसन्न करके प्रजा का पालन करते थे।
दिलीप को छोड़कर अन्य कोई भी राजा अपनी प्रजा का पालन करने में इतनी ख्याति अर्जित नहीं कर सका क्योंकि अन्य सभी राजाओं के यहां कभी, चोरी, आदि दुष्कर्म हो जाया करते थे किन्तु दिलीप के राज्य में चोरी शब्द केवल कहने-सुनने के लिए प्रयुक्त होता था, उस, राज्य में कोई किसी का धन नहीं चुराता था।
रोगी कड़वी औषधि का सेवन यह सोचकर कर लेता है क्योंकि उससे उसको रोग से छुटकारा पाने की आशा होती है। उसी प्रकार राजा दिलीप भी अपने उन वैरियों को अपना लिया करते थे जो कुछ भले होते थे। किन्तु जैसे लोग अंगुली में सांप के काटने पर लोग उसी अंगुली को ही काट कर फेंक देते हैं उसी प्रकार राजा दिलीप अपने सगे संबंधियों को भी, जो दुष्ट होते थे, निकाल कर बाहर कर देते थे।
इसमें तो कोई संदेह नहीं कि राजा दिलीप का शरीर भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच तत्त्वों से ही बना हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार ये तत्त्व निरंतर गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द रूपी गुणों से सृष्टि की सेवा करते हैं उसी प्रकार राजा दिलीप भी अपनी प्रजा की सेवा करते थे।
ज्यों कोई राजा किसी ऐसे नगर पर शासन करे जिसके चारों ओर परकोटा और खाई हो, वैसे राजा दिलीप इस सारी पृथ्वी पर एकाकी ही राज्य करते थे। इसका परकोटा समु्द्र तट था और इसकी खाई का कार्य स्वयं समुद्र करता था।
जिस प्रकार इस संसार में यज्ञ की पत्नी दक्षिणा का नाम चारों ओर प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप की भी पत्नी मगध वंश में उत्पन्न सुदक्षिणा नाम से संसार में अपनी चातुरता के लिए प्रख्यात थीं।
जिस प्रकार राजाओं के अनेक रानियां होती हैं, उसी प्रकार राजा दिलीप के भी अनेक रानियां थीं। किन्तु राजा दिलीप स्वयं को यदि पत्नीवान समझते थे तो केवल लक्ष्मी के समान मनस्विनी पत्नी सुदक्षिणा के कारण ही समझते थे।
राजा दिलीप की परम कामना यही थी कि उनकी प्रिय पत्नी सुदक्षिणा उनके समान ही तेजस्वी, ओजस्वी पुत्र को जन्म दे। किन्तु दिन बीतते जा रहे थे और राजा दिलीप का मनोरथ पूर्ण नहीं हो पा रहा था।
इससे खिन्न होकर राजा ने अपने मन में निश्चय किया कि संतान उत्पन्न करने के लिए कोई न कोई उपाय किया जाना चाहिए। यह निश्चय करने के उपरांत सर्वप्रथम राजा ने सारा राज्य कार्य अपने सुयोग्य मंत्रियों के ऊपर सौंप दिया।
जैसा कि राजा दिलीप ने अपने मन में निश्चय किया था तदनुसार, राज्य भार सौंप देने पर उन्होंने महर्षि वसिष्ठ के आश्रम में जाकर उनसे परामर्श करने का निश्चय किया। उसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी सहित प्रजापति ब्रह्मा की पूजा अर्चना की और फिर पत्नी सुदक्षिणा को लेकर वे अपने कुलगुरु महर्षि वसिष्ठ के आश्रम को गए।
जिस रथ पर वे चलकर वे जा रहे थे वह मंथर गति से मधुर घरघराहट करता हुआ चला जा रहा था। उस रथ में सवार वे दोनों ऐसे लग रहे थे मानो बादल पर ऐरावत और बिजली दोनों ही सवार होकर आकाश मार्ग से जा रहे हों।
राजा ने आश्रम जाते हुए अपने साथ कोई सेवक आदि नहीं लिए थे क्योंकि वे समझते थे कि इससे आश्रम में भीड़ अधिक होगी और आश्रम के काम में बाधा पड़ेगी। किन्तु राजा का तेज और प्रताप ही ऐसा था कि उनके अकेले चले जाने पर भी ऐसा लगता था कि मानो उनके साथ में बड़ी भारी सेना चली जा रही हो।
राजा के इस प्रकार जाते हुए पवन ऐसा लग रहा था मानो खुले मार्ग में साल की गोंद की गंध में बसा हुआ, फूलों के पराग उड़ाता हुआ और वन के वृक्षों की पांतों को धीरे-धीरे कंपाता हुआ पवन, उनके शरीर को सुख देता हुआ उनकी सेवा-सी करता हुआ मंद-मंद चला जा रहा था। राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा ने मार्ग में इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई और देखा कि कहीं-कहीं रथ की घरघराहट सुनकर बहुत-से मोर इस भ्रम से अपना मुख ऊपर उठा-उठाकर दोहरे मनोहर षडज शब्द से कूक रहे हैं कि कहीं बादल तो नहीं गरज रहे हैं ?
कहीं उन्होंने देखा कि हिरणों के जोड़े मार्ग से कुछ हटकर एकटक होकर रथ की ओर देख रहे हैं। उनकी सरल चितवन को राजा दिलीप ने सुदक्षिणा के नेत्रों के समान समझा और सुदक्षिणा ने राजा दिलीप के नेत्रों के समान।
जब कभी वे आँख उठाकर ऊपर देखते तो आकाश में उड़ते हुए और मीठे बोलने वाले बगले भी उन्हें दिखाई पड़ जाते जो पांत से उड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानों खंभे के बिना ही बंदवार टंगी हुई हो।
मार्ग में बहता हुआ पवन भी उनके अनुकूल ही चल रहा था और मानों यह संकेत दे रहा हो कि उनकी मन की आकांक्षांएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। उस समय पवन भी ऐसी दिशा से चल रहा था कि घोड़ों के खुरों से उठी हुई धूल न तो महारानी सुदक्षिणा के बालों को छू पाती थी और न राजा दिलीप की पगड़ी को ही।
आश्रम जाते हुए मार्ग में जो ताल पड़ते थे उनकी लहरों की झंकारों से उड़ती हुई कमलों की ठंडी सुगंध जिस पवन से लेते हुए वे चले जा रहे थे यह सुगंध भरा पवन उनकी सांस के समान ही सुगंधित था।
राजा ने जो गांव ब्राह्मणों को दान कर दिए थे और जिनमें स्थान-स्थान पर यज्ञवेदी के खंभे खड़े थे, वहां के ब्राह्मणों ने राजा को आते देखकर पहले तो उन्हें अर्घ्य भेंट किया और फिर उनको इस प्रकार के आशीर्वाद दिए कि जो कभी निष्फल नहीं हो सकते थे।
मार्ग में चलते हुए गावों के लोग, गाय का तुरंत निकाला हुआ मक्खन लेकर राजा को भेंट करने के लिए आगे आते थे, उनसे बातें करते हुए राजा और रानी मार्ग के आस-पास के वनों और उनमें उत्पन्न वृक्षों के नाम आदि पूछते जाते थे।
जिस प्रकार चैत्र की पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र के साथ उज्जवल चंद्रमा आँखों को भला लगता है वैसे ही सुंदरी सुदक्षिणा के साथ मार्ग में उजले वस्त्र पहने जाते हुए राजा दिलीप बड़े मनोहर लग रहे थे।
बहुत ही बुद्धिमान तथा लुभावने दिखाई देने वाले राजा दिलीप अपनी पत्नी को वे सब सुहावने दृश्य दिखाने में इतने तन्मय हो गए थे कि इसमें उन्हें यह भी भान नहीं रहा कि इतना लंबा मार्ग कब निकल गया।
इस प्रकार जाते हुए सांझ होते-होते राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ संयमी महर्षि वसिष्ठ के आश्रम तक पहुंच गए। इतने थोड़े समय में इतनी लंबी यात्रा पूरी करने के कारण उनके रथ के घोड़े भी थक गए थे।
जिस समय राजा दिलीप महर्षि के आश्रम के बाहर पहुंचे उस समय उन्होंने देखा कि महर्षि के शिष्य सायंकालीन अग्निहोत्र के लिए हाथ में समिधा, कुशा और फल लिए हुए वन से लौट रहे हैं।
उस समय आश्रम के इधर-उधर पर्णकुटियों के बाहर के द्वार पर बहुत-से मृग आकर इस प्रकार खड़े हो गए थे मानो द्वार से किसी को भीतर न जाने देना चाहते हों। क्योंकि उन मृगों को भी ऋषि पत्नियों के बालकों के समान ही तिन्नी के दाने खाने का अभ्यास पड़ गया था।
जिस समय राजा दिलीप आश्रम के निकट पहुंचे तब तक ऋषि कन्याएं वृक्षों के जड़ों को पानी से सींच चुकी थी। और उनके जाने के बाद आश्रम के पक्षी उन जड़ों में एकत्रित जल को निशंक होकर पीते हुए जल में ही केलि कर रहे थे।
तिन्नी का जो अन्न धूप में सुखाने के लिए फैलाया हुआ था वह अब दिन छिपने के कारण समेट लिया गया था और उसे कुटिया के आंगन में एकत्रित करके रख दिया गया था। उसके समीप ही आंगन में बैठे हिरण बड़े आराम से जुगाली कर रहे थे।
अग्निहोत्र का धुंआ, हवन सामग्री की गंध से भरा हुआ पवन के साथ-साथ आश्रम के चारों ओर फैल गया था, उस धुंए ने आश्रम की ओर आते हुए इन अतिथि अर्थात राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा को भी पवित्र कर दिया।
उस समय राजा दिलीप ने अपने सारथि को कहा कि वह अब रथ को रोक कर घोड़ों को विश्राम दे। रथ के रुकने पर पहले राजा ने अपने हाथ के आश्रय से अपनी पत्नी को रथ से उतारा और फिर उसके बाद वे स्वयं रथ से उतर गए।
आश्रमवासियों को जब राजा और रानी के आने का समाचार प्राप्त हुआ तो वहां के सभ्य एवं संयमी मुनियों ने अपने रक्षक, आदरणीय तथा नीति के अनुसार चलने वाले राजा का सपत्नीक सम्मान के साथ आश्रम में स्वागत किया।
आश्रम में प्रविष्ट होने पर वहां उन्होंने संध्या की सब क्रियाएं पूर्ण की। इसी प्रकार सब आश्रमवासियों की सब सांध्य क्रियाएं सम्पन्न होने के बाद महाराज और महारानी उन तपस्वी महामुनि वसिष्ठ के समीप वहां पर गए जहां वे बैठे हुए थे। उनके पीछे उनकी पत्नी अरुन्धती भी इस प्रकार बैठी थीं जिस प्रकार अग्नि के पीछे स्वाहा।
उनके समीप पहुंचने पर राजा और उनकी पत्नी मगधकुमारी सुदक्षिणा ने कुलगुरु तथा उनकी पत्नी के चरण स्पर्श कर उनको प्रणाम किया। महर्षि वसिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधती ने हृदय से उनको आशीर्वाद प्रदान कर आनंदित किया और बड़े प्यार तथा दुलार से उनका स्वागत किया।
प्रणामानंतर महर्षि वसिष्ठ ने राजा और रानी का इस प्रकार सत्कार किया कि जिससे मार्ग में चलते हुए रथ के हिचकोलों से शरीर क्लांत हो गया था वह प्रफुल्लित हो गया। इस प्रकार सब क्रियाओं से निवृत्त होने के उपरांत महर्षि वसिष्ठ ने राजा दिलीप से पूछा-
‘राजन् ! आपके राज्य में सब प्रकार से कुशल तो है न ?’
राजा दिलीप ने केवल शस्त्रास्त्र विद्या के संचालन में ही निपुण थे, न केवल अपनी वीरता से ही उन्होंने अनेकानेक नगर जीते थे, वे बातचीत में भी उतने ही कुशल थे। इसलिए अथर्ववेद के रक्षक वसिष्ठ जी से उनके प्रश्न के उत्तर में बड़ी अर्थभरी वाणी में उन्होंने कहा-
गुरुदेव ! आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग-राजा, मंत्री, मित्र, राजकोष, राज्य, दुर्ग और सेना सब परिपूर्ण हैं। अग्नि, जल, महामारी और अकाल-मृत्यु इन देवी विपत्तियों तथा चोर, डाकू शत्रु आदि मानुषी आपत्तियों को दूर करने वाले तो आप यहां प्रत्यक्ष विराजमान हैं।
आप मंत्रों के रचयिता हैं, आपके मंत्र ही इतने शक्तिशाली हैं कि मुझे बाण चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि अपने वाणों से तो मैं केवल उनको वेध ही सकता हूं जो कि मेरी सम्मुख आते हैं, परन्तु आपके मंत्र तो यहीं से मेरे शत्रुओं का नाश कर देते हैं।
महामुनि ! आप जब शास्त्रीय विधि से अग्नि में हवि छोड़ते हैं तो आपकी आहुतियां अनावृष्टि से सूखे हुए धान के खेतों पर जल वृष्टि के रूप में बरसने लगते हैं।
यह आपके ही के ब्रह्म के तेज का बल है कि मेरे राज्य में न तो कोई सौ वर्ष से कम की आयु पाता है और न किसी को- बाढ़, सूखा, चूहा, तोता, राजकलह, वैरी की चढ़ाई आदि तथा विपत्ति का भय रहता है।
एक बात और, मैं हूं तो मंदबुद्धि वाला व्यक्ति किंतु मेरी साध यह है कि प्रख्यात कवियों के समान मुझे भी यश प्राप्त हो। लोग यदि मेरे इस साध के विषय में सुनेंगे तो मुझ पर बहुत हंसेंगे। क्योंकि इस संबंध में मेरी स्थिति ठीक उस बौने व्यक्ति के समान है जो दूर ऊंचे पेंड़ पर लगे उन फलों को तोड़ने के लिए साध लिए हो जिनको केवल लंबे व्यक्ति और लंबे हाथ वाले ही पा सकते हैं।
किंतु इसमें भी एक संतोष की बात यह है कि पूर्व काल में महर्षि वाल्मीक आदि महान कवियों ने उनके विषय में सुंदर काव्य लिख करके मेरे लिए वाणी का द्वार खोल दिया है। इसलिए इस विषय की पैठ अब मेरे लिए सरल हो गई है, यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कि मोतियों को पहले ही बांध दिया हो, उसमें फिर सुई से धागा पिरोना बहुत ही सुगम हो जाता है।
जैसा कि मैंने आरंभ में ही कह दिया है कि मैं नितांत मंदमति हूं, मुझे कुछ आता-जाता नहीं। फिर भी मैं उन रघुवंशियों का वर्णन करने के लिए समुद्यत हूं-
जिनके चरित्र जन्म से आरंभ करके अंत तक शुद्ध और पवित्र रहे हैं, जो किसी काम का जब बीड़ा उठाते थे उसको पूर्ण करके ही विराम लेते थे, जो समुद्र के ओर-छोर तक फैली हुई यह धरती है, उसके स्वामी थे और जिनके रथ पृथ्वी से स्वर्ग तक सीधे जाया करते थे।
जो नित्य नियम पूर्वक शास्त्रों की विधि से यज्ञ किया करते थे, जो याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार मुंह-मांगा और मनचाहा दान दिया करते थे, जो अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार ही दंड देते थे और जो अवसर देखकर ही तदनुरूप कार्य किया करते थे।
जो रघुवंशी केवल त्याग के लिए, दान करने के लिए ही धन का संग्रह किया करते थे, और जो सत्य के पालन के लिए बहुत कम बोला करते थे। अभिप्राय यह है कि जितना कहा जाए उसका अक्षरशः पालन किया जाए, जो केवल यश प्राप्ति के लिए ही अन्य देशों को जीतते थे, उन राज्यों को अपने वश में करने अथवा वहां लूटपाट करने के लिए नहीं और जो केवल प्रजा के लिए अर्थात अपनी संतान प्राप्ति के लिए ही गृहस्थ में प्रविष्ट होते थे, भोग विलास के लिए नहीं।
जो बाल्यकाल में सभी को अध्ययन कर उनमें पारंगत होते थे और तरुणाई में संसार के भोगों का आनन्द लेते थे। इसके उपरांत तृतीयावस्था में वनों में जाकर मुनिवृत्ति धारण करते हुए तपस्या करते थे और अंत में ब्रह्म अथवा परमात्मा का ध्यान करते हुए योग द्वारा पार्थिव शरीर को शांत करते थे
इस प्रकार के जो रघुवंशी थे, इन गुणों से संपन्न जो वंश था, उससे ही प्रभावित होकर मैं यह काव्य लिखने के लिए प्रेरित हुआ हूं।
इस काव्य को, अर्थात रघुकुल के इस गुणानुवाद को सुनने के अधिकारी भी वे ही संत सज्जन हो सकते हैं, जिनमें भले-बुरे की परख की योग्यता है।
क्योंकि सोना खरा है अथवा खोटा इसका पता तो तब ही लग सकता है जब उसको अग्नि में तपाया जाए।
अब मैं उस वंश का वर्णन करता हूं-
जिस प्रकार वेद के छंदों में सर्वप्रथम आकार के लिए स्थान है उसी प्रकार राजाओं में सर्वप्रथम सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए हैं। मनु महाराज बड़े मनीषि थे और मनीषियों में बड़े माननीय और आदरणीय माने जाते थे।
उन्हीं वैवस्वत मनु के उज्जवल वंश में चन्द्रमा के समान सबको सुख प्रदान करने वाले और बहुत ही शुद्ध चरित्र वाले राजा दिलीप ने जन्म लिया। उनके जन्म से ऐसा लगा मानों क्षीर सागर में चंद्रमा ने जन्म लिया हो।
राजा दिलीप के शरीर सौष्ठव का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं-
दिलीप का रूप देखने योग्य था उनकी छाती खूब चौड़ी थी। वे वृषस्कंध अर्थात सांड के समान चौड़े कंधों वाले थे, उनकी भुजाएं शाल के वृक्ष के समान लम्बी-लम्बी थीं। उनका अपार तेज देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो क्षत्रियों का जो वीरत्व धर्म है उनके शरीर में यह समझ कर प्रविष्ट हो गया हो कि सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों के संहार करने का जो उसका काम है वह इस शरीर के माध्यम से अवश्य पूर्ण हो सकेगा।
जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता से संसार के सब दृढ़ पदार्थों को दबा लिया है और अपनी चमक से उसने सब चमकीली वस्तुओं की चमक को घटा दिया है, तथा अपनी ऊंचाई से सब ऊंची वस्तुओं को नीचा कर दिया है एवं अपने विस्तार से सारी पृथ्वी को ढक लिया है। ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप ने अपने बल, तेज और सुदृढ़ शरीर से सबको एक प्रकार से विजित-सा करके सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया है।
जैसा उनका सुंदर रूप था ठीक उसी प्रकार उनकी बुद्धि भी थी और जैसी उनकी तीव्र बुद्धि थी उसके अनुसार उन्होंने शीघ्र ही सब शास्त्रों को पढ़ लिया था। इसलिए वे शास्त्रानुसार ही अपना कार्य करते थे इसलिए उनको तदनुरूप ही सफलता भी प्राप्त होती थी।
जिस प्रकार समुद्री भयानक जंतु मगर तथा घड़ियाल आदि के भय से लोग समुद्र में प्रविष्ट होने से डरते हैं, वैसे ही राजा दिलीप के सेवक आदि उनसे डरते थे। उसका मुख्य कारण यह था कि वे न्याय करने में बड़े कठोर थे, वे किसी का पक्षपात नहीं करते थे। किन्तु समुद्र के सुंदर रत्नों की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार लोग समुद्र में प्रविष्ट होते हैं ठीक उसी प्रकार दयालु, उदार, गुणवान, राजा दिलीप की कृपा पाने के लिए उनके सेवक सदा उनका मुख भी जोहते रहते थे।
ज्यों चतुर सारथी जिस प्रकार रथ चलाता है उस समय उसके रथ के पहिए बाल भर भी लीक से बाहर नहीं हो पाते, उस प्रकार राजा दिलीप ने प्रजा की भी ऐसी पालना की कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति मनु द्वारा निर्दिष्ट नियमों से बाल भर भी बाहर नहीं जाता था। सब लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रम में रहते हुए अपने-अपने धर्म का यथावत पालन करते थे।
जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जल शोख कर फिर वर्षा के रूप में उससे अनेक गुणा अधिक उसको ही प्रदान करता है उसी प्रकार राजा दिलीप भी प्रजा से राजस्व प्राप्त करके फिर प्रजा की भलाई में उसको व्यय कर देते थे। प्रजा की भलाई के लिए ही वे प्रजा से ही कर लिया करते थे।
परंपरा के अनुसार जिस प्रकार अन्याय राजाओं के पास बड़ी-बड़ी सेनाएं होती हैं उसी प्रकार राजा दिलीप की यह सेना केवल शोभा के लिए ही थी स्वयं राजा दिलीप जितने शास्त्रों में निष्णात थे। उतने ही वे धनुर्विद्या में भी निपुण थे। इसलिए अपना सारा कार्य वे अपनी चतुर बुद्धि और धनुष पर चढ़ी डोरी से ही निकाल लिया करते थे।
राजा दिलीप न तो किसी को अपने मन का भेद बताते थे और न अपनी भंगिमाओं से अपने मन की बात किसी को जानने देते थे। जैसे किसी व्यक्ति के इस जन्म के जीवन में उसके सुखी अथवा दुखी देखकर लोग यह अनुमान लगाने लगते हैं उसने पिछले जन्म में उसी प्रकार के अच्छे अथवा बुरे कर्म किए होंगे वैसे ही राजा दिलीप के मन की बात भी लोग तभी जान पाते थे जब कि वह किसी कार्य को संपन्न कर लेते थे।
राजा दिलीप निडर होकर अपनी रक्षा करते थे, बड़े धीरज के साथ वे अपने धर्म का पालन करते थे, धन एकत्रित करने में उनको किसी प्रकार का लोभ नहीं सताता थ, लोभ का त्याग करके ही वे धन का संग्रह करते थे, इसी प्रकार के संसार के सुख का भी उनमें किसी प्रकार का मोह नहीं था।
मनुष्य में यदि किसी प्रकार का कोई गुण हुआ तो वह उसका बखान करता फिरता है। वीर वीरता का, दानी अपने दान का, विद्वान अपनी विद्या को आदि आदि, जिससे कि संसार में उसका नाम हो सके। किन्तु राजा दिलीप का स्वभाव ऐसा नहीं था। वे सब कुछ जान कर भी चुप रहते थे अर्थात अपनी विद्वता का ढिढोरा नहीं पीटते थे, शत्रुओं को जहां तक संभव होता था, वे क्षमा कर दिया करते थे, दान देकर भी कभी उन्होंने उसके विषय में बखान नहीं किया। उनके इस प्रकार के निराले व्यवहार को देखकर ऐसा अनुभव होता था कि चुप रहने, क्षमा करने और प्रशंसा से दूर भागने के गुण भी उनमें ज्ञान, शक्ति और त्याग के साथ ही उत्पन्न हुए थे।
राजा दिलीप संसार के भोगों को अपने पास फटकने नहीं देते थे। सारी विद्याओं में वे निष्णात थे। उनका अपना सारा जीवन दिन-रात धर्म में ही लगा रहता था। इस प्रकार छोटी-सी अवस्था में भी वे इतने निपुण और इतने चतुर हो गए थे कि बुढ़ापा आए बिना भी उनकी गणना बूढ़ों में होने लगी थी। अर्थात उनको परिपक्व बुद्धि का प्रौढ़ व्यक्ति माना जाता था।
पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रों को बुरा काम करने से रोके और शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त करे, सब प्रकार से उनका पालन-पोषण और रक्षा करता हुआ उन्हें योग्य बनाए। ठीक उसी प्रकार महाराजा दिलीप भी अपनी प्रजा का पुत्रवत् पालन करते हुए उसका भरण-पोषण करते थे और विपत्ति से उनकी रक्षा करते थे अर्थात सब प्रकार से उनका संरक्षण करते थे। इस प्रकार पिता तो केवल जन्म देने वाले ही थे वास्तव में राजा दिलीप ही सब प्रकार से उसके पिता समान थे।
राजा का धर्म है कि वह अपराधी को दंडित करे, इसके बिना राज्यस्थिर नहीं रहता। इसलिए वे अपराधियों को अवश्य दंड देते थे। संतान उत्पन्न करके वंश चलाने के लिए ही उन्होंने विवाह किया था। भोग विलास के लिए नहीं। इस प्रकार दंड और विवाह यद्यपि अर्थ और काम शास्त्र के विषय है फिर भी राजा के हाथों में पहुंचकर वे धर्म ही बन गए थे।
वे प्रजा से जो कर लिया करते थे उसको वे इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में लगा दिया करते थे। इस प्रकार इन्द्र उनसे प्रसन्न होकर आकाश से उनकी प्रजा पर दृष्टि रखता था, इस प्रकार उनके राज्य में खूब खेती लहलहाती थी। राजा दिलीप और इंद्र एक दूसरे को प्रसन्न करके प्रजा का पालन करते थे।
दिलीप को छोड़कर अन्य कोई भी राजा अपनी प्रजा का पालन करने में इतनी ख्याति अर्जित नहीं कर सका क्योंकि अन्य सभी राजाओं के यहां कभी, चोरी, आदि दुष्कर्म हो जाया करते थे किन्तु दिलीप के राज्य में चोरी शब्द केवल कहने-सुनने के लिए प्रयुक्त होता था, उस, राज्य में कोई किसी का धन नहीं चुराता था।
रोगी कड़वी औषधि का सेवन यह सोचकर कर लेता है क्योंकि उससे उसको रोग से छुटकारा पाने की आशा होती है। उसी प्रकार राजा दिलीप भी अपने उन वैरियों को अपना लिया करते थे जो कुछ भले होते थे। किन्तु जैसे लोग अंगुली में सांप के काटने पर लोग उसी अंगुली को ही काट कर फेंक देते हैं उसी प्रकार राजा दिलीप अपने सगे संबंधियों को भी, जो दुष्ट होते थे, निकाल कर बाहर कर देते थे।
इसमें तो कोई संदेह नहीं कि राजा दिलीप का शरीर भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच तत्त्वों से ही बना हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार ये तत्त्व निरंतर गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द रूपी गुणों से सृष्टि की सेवा करते हैं उसी प्रकार राजा दिलीप भी अपनी प्रजा की सेवा करते थे।
ज्यों कोई राजा किसी ऐसे नगर पर शासन करे जिसके चारों ओर परकोटा और खाई हो, वैसे राजा दिलीप इस सारी पृथ्वी पर एकाकी ही राज्य करते थे। इसका परकोटा समु्द्र तट था और इसकी खाई का कार्य स्वयं समुद्र करता था।
जिस प्रकार इस संसार में यज्ञ की पत्नी दक्षिणा का नाम चारों ओर प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप की भी पत्नी मगध वंश में उत्पन्न सुदक्षिणा नाम से संसार में अपनी चातुरता के लिए प्रख्यात थीं।
जिस प्रकार राजाओं के अनेक रानियां होती हैं, उसी प्रकार राजा दिलीप के भी अनेक रानियां थीं। किन्तु राजा दिलीप स्वयं को यदि पत्नीवान समझते थे तो केवल लक्ष्मी के समान मनस्विनी पत्नी सुदक्षिणा के कारण ही समझते थे।
राजा दिलीप की परम कामना यही थी कि उनकी प्रिय पत्नी सुदक्षिणा उनके समान ही तेजस्वी, ओजस्वी पुत्र को जन्म दे। किन्तु दिन बीतते जा रहे थे और राजा दिलीप का मनोरथ पूर्ण नहीं हो पा रहा था।
इससे खिन्न होकर राजा ने अपने मन में निश्चय किया कि संतान उत्पन्न करने के लिए कोई न कोई उपाय किया जाना चाहिए। यह निश्चय करने के उपरांत सर्वप्रथम राजा ने सारा राज्य कार्य अपने सुयोग्य मंत्रियों के ऊपर सौंप दिया।
जैसा कि राजा दिलीप ने अपने मन में निश्चय किया था तदनुसार, राज्य भार सौंप देने पर उन्होंने महर्षि वसिष्ठ के आश्रम में जाकर उनसे परामर्श करने का निश्चय किया। उसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी सहित प्रजापति ब्रह्मा की पूजा अर्चना की और फिर पत्नी सुदक्षिणा को लेकर वे अपने कुलगुरु महर्षि वसिष्ठ के आश्रम को गए।
जिस रथ पर वे चलकर वे जा रहे थे वह मंथर गति से मधुर घरघराहट करता हुआ चला जा रहा था। उस रथ में सवार वे दोनों ऐसे लग रहे थे मानो बादल पर ऐरावत और बिजली दोनों ही सवार होकर आकाश मार्ग से जा रहे हों।
राजा ने आश्रम जाते हुए अपने साथ कोई सेवक आदि नहीं लिए थे क्योंकि वे समझते थे कि इससे आश्रम में भीड़ अधिक होगी और आश्रम के काम में बाधा पड़ेगी। किन्तु राजा का तेज और प्रताप ही ऐसा था कि उनके अकेले चले जाने पर भी ऐसा लगता था कि मानो उनके साथ में बड़ी भारी सेना चली जा रही हो।
राजा के इस प्रकार जाते हुए पवन ऐसा लग रहा था मानो खुले मार्ग में साल की गोंद की गंध में बसा हुआ, फूलों के पराग उड़ाता हुआ और वन के वृक्षों की पांतों को धीरे-धीरे कंपाता हुआ पवन, उनके शरीर को सुख देता हुआ उनकी सेवा-सी करता हुआ मंद-मंद चला जा रहा था। राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा ने मार्ग में इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई और देखा कि कहीं-कहीं रथ की घरघराहट सुनकर बहुत-से मोर इस भ्रम से अपना मुख ऊपर उठा-उठाकर दोहरे मनोहर षडज शब्द से कूक रहे हैं कि कहीं बादल तो नहीं गरज रहे हैं ?
कहीं उन्होंने देखा कि हिरणों के जोड़े मार्ग से कुछ हटकर एकटक होकर रथ की ओर देख रहे हैं। उनकी सरल चितवन को राजा दिलीप ने सुदक्षिणा के नेत्रों के समान समझा और सुदक्षिणा ने राजा दिलीप के नेत्रों के समान।
जब कभी वे आँख उठाकर ऊपर देखते तो आकाश में उड़ते हुए और मीठे बोलने वाले बगले भी उन्हें दिखाई पड़ जाते जो पांत से उड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानों खंभे के बिना ही बंदवार टंगी हुई हो।
मार्ग में बहता हुआ पवन भी उनके अनुकूल ही चल रहा था और मानों यह संकेत दे रहा हो कि उनकी मन की आकांक्षांएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। उस समय पवन भी ऐसी दिशा से चल रहा था कि घोड़ों के खुरों से उठी हुई धूल न तो महारानी सुदक्षिणा के बालों को छू पाती थी और न राजा दिलीप की पगड़ी को ही।
आश्रम जाते हुए मार्ग में जो ताल पड़ते थे उनकी लहरों की झंकारों से उड़ती हुई कमलों की ठंडी सुगंध जिस पवन से लेते हुए वे चले जा रहे थे यह सुगंध भरा पवन उनकी सांस के समान ही सुगंधित था।
राजा ने जो गांव ब्राह्मणों को दान कर दिए थे और जिनमें स्थान-स्थान पर यज्ञवेदी के खंभे खड़े थे, वहां के ब्राह्मणों ने राजा को आते देखकर पहले तो उन्हें अर्घ्य भेंट किया और फिर उनको इस प्रकार के आशीर्वाद दिए कि जो कभी निष्फल नहीं हो सकते थे।
मार्ग में चलते हुए गावों के लोग, गाय का तुरंत निकाला हुआ मक्खन लेकर राजा को भेंट करने के लिए आगे आते थे, उनसे बातें करते हुए राजा और रानी मार्ग के आस-पास के वनों और उनमें उत्पन्न वृक्षों के नाम आदि पूछते जाते थे।
जिस प्रकार चैत्र की पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र के साथ उज्जवल चंद्रमा आँखों को भला लगता है वैसे ही सुंदरी सुदक्षिणा के साथ मार्ग में उजले वस्त्र पहने जाते हुए राजा दिलीप बड़े मनोहर लग रहे थे।
बहुत ही बुद्धिमान तथा लुभावने दिखाई देने वाले राजा दिलीप अपनी पत्नी को वे सब सुहावने दृश्य दिखाने में इतने तन्मय हो गए थे कि इसमें उन्हें यह भी भान नहीं रहा कि इतना लंबा मार्ग कब निकल गया।
इस प्रकार जाते हुए सांझ होते-होते राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ संयमी महर्षि वसिष्ठ के आश्रम तक पहुंच गए। इतने थोड़े समय में इतनी लंबी यात्रा पूरी करने के कारण उनके रथ के घोड़े भी थक गए थे।
जिस समय राजा दिलीप महर्षि के आश्रम के बाहर पहुंचे उस समय उन्होंने देखा कि महर्षि के शिष्य सायंकालीन अग्निहोत्र के लिए हाथ में समिधा, कुशा और फल लिए हुए वन से लौट रहे हैं।
उस समय आश्रम के इधर-उधर पर्णकुटियों के बाहर के द्वार पर बहुत-से मृग आकर इस प्रकार खड़े हो गए थे मानो द्वार से किसी को भीतर न जाने देना चाहते हों। क्योंकि उन मृगों को भी ऋषि पत्नियों के बालकों के समान ही तिन्नी के दाने खाने का अभ्यास पड़ गया था।
जिस समय राजा दिलीप आश्रम के निकट पहुंचे तब तक ऋषि कन्याएं वृक्षों के जड़ों को पानी से सींच चुकी थी। और उनके जाने के बाद आश्रम के पक्षी उन जड़ों में एकत्रित जल को निशंक होकर पीते हुए जल में ही केलि कर रहे थे।
तिन्नी का जो अन्न धूप में सुखाने के लिए फैलाया हुआ था वह अब दिन छिपने के कारण समेट लिया गया था और उसे कुटिया के आंगन में एकत्रित करके रख दिया गया था। उसके समीप ही आंगन में बैठे हिरण बड़े आराम से जुगाली कर रहे थे।
अग्निहोत्र का धुंआ, हवन सामग्री की गंध से भरा हुआ पवन के साथ-साथ आश्रम के चारों ओर फैल गया था, उस धुंए ने आश्रम की ओर आते हुए इन अतिथि अर्थात राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा को भी पवित्र कर दिया।
उस समय राजा दिलीप ने अपने सारथि को कहा कि वह अब रथ को रोक कर घोड़ों को विश्राम दे। रथ के रुकने पर पहले राजा ने अपने हाथ के आश्रय से अपनी पत्नी को रथ से उतारा और फिर उसके बाद वे स्वयं रथ से उतर गए।
आश्रमवासियों को जब राजा और रानी के आने का समाचार प्राप्त हुआ तो वहां के सभ्य एवं संयमी मुनियों ने अपने रक्षक, आदरणीय तथा नीति के अनुसार चलने वाले राजा का सपत्नीक सम्मान के साथ आश्रम में स्वागत किया।
आश्रम में प्रविष्ट होने पर वहां उन्होंने संध्या की सब क्रियाएं पूर्ण की। इसी प्रकार सब आश्रमवासियों की सब सांध्य क्रियाएं सम्पन्न होने के बाद महाराज और महारानी उन तपस्वी महामुनि वसिष्ठ के समीप वहां पर गए जहां वे बैठे हुए थे। उनके पीछे उनकी पत्नी अरुन्धती भी इस प्रकार बैठी थीं जिस प्रकार अग्नि के पीछे स्वाहा।
उनके समीप पहुंचने पर राजा और उनकी पत्नी मगधकुमारी सुदक्षिणा ने कुलगुरु तथा उनकी पत्नी के चरण स्पर्श कर उनको प्रणाम किया। महर्षि वसिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधती ने हृदय से उनको आशीर्वाद प्रदान कर आनंदित किया और बड़े प्यार तथा दुलार से उनका स्वागत किया।
प्रणामानंतर महर्षि वसिष्ठ ने राजा और रानी का इस प्रकार सत्कार किया कि जिससे मार्ग में चलते हुए रथ के हिचकोलों से शरीर क्लांत हो गया था वह प्रफुल्लित हो गया। इस प्रकार सब क्रियाओं से निवृत्त होने के उपरांत महर्षि वसिष्ठ ने राजा दिलीप से पूछा-
‘राजन् ! आपके राज्य में सब प्रकार से कुशल तो है न ?’
राजा दिलीप ने केवल शस्त्रास्त्र विद्या के संचालन में ही निपुण थे, न केवल अपनी वीरता से ही उन्होंने अनेकानेक नगर जीते थे, वे बातचीत में भी उतने ही कुशल थे। इसलिए अथर्ववेद के रक्षक वसिष्ठ जी से उनके प्रश्न के उत्तर में बड़ी अर्थभरी वाणी में उन्होंने कहा-
गुरुदेव ! आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग-राजा, मंत्री, मित्र, राजकोष, राज्य, दुर्ग और सेना सब परिपूर्ण हैं। अग्नि, जल, महामारी और अकाल-मृत्यु इन देवी विपत्तियों तथा चोर, डाकू शत्रु आदि मानुषी आपत्तियों को दूर करने वाले तो आप यहां प्रत्यक्ष विराजमान हैं।
आप मंत्रों के रचयिता हैं, आपके मंत्र ही इतने शक्तिशाली हैं कि मुझे बाण चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि अपने वाणों से तो मैं केवल उनको वेध ही सकता हूं जो कि मेरी सम्मुख आते हैं, परन्तु आपके मंत्र तो यहीं से मेरे शत्रुओं का नाश कर देते हैं।
महामुनि ! आप जब शास्त्रीय विधि से अग्नि में हवि छोड़ते हैं तो आपकी आहुतियां अनावृष्टि से सूखे हुए धान के खेतों पर जल वृष्टि के रूप में बरसने लगते हैं।
यह आपके ही के ब्रह्म के तेज का बल है कि मेरे राज्य में न तो कोई सौ वर्ष से कम की आयु पाता है और न किसी को- बाढ़, सूखा, चूहा, तोता, राजकलह, वैरी की चढ़ाई आदि तथा विपत्ति का भय रहता है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book