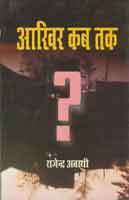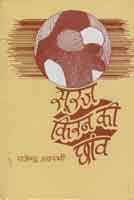|
लेख-निबंध >> आखिर कब तक आखिर कब तकराजेन्द्र अवस्थी
|
401 पाठक हैं |
||||||
राजेन्द्र अवस्थी के द्वारा चुने हुए कुछ छोटे-छोटे आलेखों का वर्णन...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
राजेन्द्र अवस्थी कथाकार और पत्रकार तो हैं ही, उन्होंने सांस्कृतिक
राजनीति तथा सामयिक विषयों पर भी भरपूर लिखा है। अनेक दैनिक समाचार-पत्रों
तथा पत्रिकाओं में उनके लेख प्रमुखता से छपते रहे। उनकी बेबाक टिप्पणियाँ
अनेक बार आक्रोश और विवाद को भी जन्म देती रहीं, लेकिन अवस्थी जी कभी भी
अपनी बात कहने से नहीं चूकते। वह कहेंगे और निडर तथा बेबाक होकर कहेंगे
भले ही उनके मित्र उनसे अप्रसन्न क्यों न हो जाएँ। परिणामस्वरूप, उनका यह
लेखन समसामयिक साहित्य का दस्तावेज बन गया। उन्होंने कई सुविख्यात
व्यक्तित्वों के जीवन को आधार बनाकर औपन्यासिक कृतियाँ दी हैं और उनमें
कथानायकों की विशेषताओं के साथ ही उनकी दुर्बलताओं की चर्चा भी की है।
सक्रिय लेखन के दौरान बड़ी-बड़ी हस्तियों से उनका साबका तो पड़ता ही रहा।
यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि कई बड़े लोगों के वह आत्मीय रहे हैं। ऐसे
लेखन से उनका क्षेत्र व्यापक बना और साहित्य के रचना-प्रदेश के बाहर भी
अन्य क्षेत्रों में उनकी खासी सर्जनात्मक पहचान बन गई।
प्रस्तुत टिप्पणियाँ मूल्यवान लेखन है। लेखक का मानना है कि उन्होंने एक भी घटना न बनावटी लिखी है और न ही कभी झूठ-फरेबी पत्रकारिता को स्वीकारा। जो जैसा है जो सही है, जो स्पंदित है उसी पर उन्होंने लिखा है। इस दृष्टि से यह कृति अत्यंत महत्वपूर्ण हो उठती है।
प्रस्तुत टिप्पणियाँ मूल्यवान लेखन है। लेखक का मानना है कि उन्होंने एक भी घटना न बनावटी लिखी है और न ही कभी झूठ-फरेबी पत्रकारिता को स्वीकारा। जो जैसा है जो सही है, जो स्पंदित है उसी पर उन्होंने लिखा है। इस दृष्टि से यह कृति अत्यंत महत्वपूर्ण हो उठती है।
राजेन्द्र अवस्थीः एक सजग प्रहरी
स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी ने जितने
प्रयोग किए हैं, शायद ही किसी
अन्य भारतीय कथा साहित्य में हुए हों। राजेन्द्र प्रसाद उन्हीं
प्रयोगधर्मी कथाकारों में शीर्ष श्रेणी के कथा-शिल्पी हैं। भाषा, भाव,
शैली और वस्तु-विन्यास तथा कथानक के चुनाव में उनका विशिष्ट स्थान है।
राजेन्द्र अवस्थी की अब तक साठ से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रा-वृत्तांत के साथ-साथ उनका दार्शनिक स्वरूप है जो शायद ही किसी कथाकार में देखने को मिलता है। श्री अवस्थी विश्व-यात्री हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहाँ अनेक बार वे न गए हों। वहाँ के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के साथ उनका पूरा समन्वय रहा है।
राजेन्द्र अवस्थी को शीर्षतम सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अनेक राज्य सरकारों के सर्वोच्च पुरस्कार भी मिले हैं। देश-विदेश में उनकी ख्याति और वहाँ से प्राप्त सम्मान उन्हें हिंदी जगत् में विशेष स्थान से समादृत करने के लिए पर्याप्त हैं।
अवस्थी जी को भारत और विदेशों के कुछ विश्वविद्यालयों से ‘डॉक्टर ऑफ लिटरेचर’ की मानद उपाधि मिल चुकी है। अब तक 140 से अधिक शोधार्थी उन पर शोध कर चुके हैं।
राजेन्द्र अवस्थी देश के शीर्षतम पत्रकार, संपादक : ‘कादंबिनी’, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली। भूतपूर्व संपादक : ‘सारिका’, ‘नंदन’ और ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’। उनकी हर टिप्पणी अत्यंत सत्य और सजग है।
अपनी इस यायावरी प्रवृत्ति को लेकर श्री अवस्थी ने अपने आत्मकथात्मक आलेख में स्वयं बहुत कुछ लिखा है। हम उसके विस्तार में नहीं जाना चाहते। फिर भी उनकी एक बात सदा स्मरण रहती है कि लंदन, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क की सड़कों, उपसड़कों का उन्होंने इतनी बार भ्रमण किया है कि इन स्थानों पर उन्हें अकेले छोड़ दिया जाए तो वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचकर रहेंगे।
अवस्थी जी की विशेषता यह है कि साहित्यिक पत्रकारिता के मानदंड के रूप में वे हमेशा ख्यात रहेंगे। श्री अवस्थी के ‘कालचिंतन’ ने पाठकों के श्रवण रंध्रों में प्रतिमाह पीयूष-प्रवाह उड़लने का पुनीत कार्य किया है।
श्री अवस्थी सर्वप्रथम एक श्रेष्ठ रचनाधर्मी हैं और उनकी इसी रचनाधर्मिता ने उनकी पत्रकारिता (साहित्यिक) को वह धार दी है जिस पर चलने की क्षमता सब में नहीं है। उपनिषद् ऋषि के शब्दों में :
राजेन्द्र अवस्थी की अब तक साठ से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रा-वृत्तांत के साथ-साथ उनका दार्शनिक स्वरूप है जो शायद ही किसी कथाकार में देखने को मिलता है। श्री अवस्थी विश्व-यात्री हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहाँ अनेक बार वे न गए हों। वहाँ के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के साथ उनका पूरा समन्वय रहा है।
राजेन्द्र अवस्थी को शीर्षतम सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अनेक राज्य सरकारों के सर्वोच्च पुरस्कार भी मिले हैं। देश-विदेश में उनकी ख्याति और वहाँ से प्राप्त सम्मान उन्हें हिंदी जगत् में विशेष स्थान से समादृत करने के लिए पर्याप्त हैं।
अवस्थी जी को भारत और विदेशों के कुछ विश्वविद्यालयों से ‘डॉक्टर ऑफ लिटरेचर’ की मानद उपाधि मिल चुकी है। अब तक 140 से अधिक शोधार्थी उन पर शोध कर चुके हैं।
राजेन्द्र अवस्थी देश के शीर्षतम पत्रकार, संपादक : ‘कादंबिनी’, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली। भूतपूर्व संपादक : ‘सारिका’, ‘नंदन’ और ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’। उनकी हर टिप्पणी अत्यंत सत्य और सजग है।
अपनी इस यायावरी प्रवृत्ति को लेकर श्री अवस्थी ने अपने आत्मकथात्मक आलेख में स्वयं बहुत कुछ लिखा है। हम उसके विस्तार में नहीं जाना चाहते। फिर भी उनकी एक बात सदा स्मरण रहती है कि लंदन, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क की सड़कों, उपसड़कों का उन्होंने इतनी बार भ्रमण किया है कि इन स्थानों पर उन्हें अकेले छोड़ दिया जाए तो वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचकर रहेंगे।
अवस्थी जी की विशेषता यह है कि साहित्यिक पत्रकारिता के मानदंड के रूप में वे हमेशा ख्यात रहेंगे। श्री अवस्थी के ‘कालचिंतन’ ने पाठकों के श्रवण रंध्रों में प्रतिमाह पीयूष-प्रवाह उड़लने का पुनीत कार्य किया है।
श्री अवस्थी सर्वप्रथम एक श्रेष्ठ रचनाधर्मी हैं और उनकी इसी रचनाधर्मिता ने उनकी पत्रकारिता (साहित्यिक) को वह धार दी है जिस पर चलने की क्षमता सब में नहीं है। उपनिषद् ऋषि के शब्दों में :
सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया।
दुर्गमपथस्तत कवयो वदन्ति।।
दुर्गमपथस्तत कवयो वदन्ति।।
श्री अवस्थी का एक आयाम और भी
है—उनका अत्यंत स्नेहिल, कृतज्ञ,
संवेदनशील और सुहृद होना। इस सरल सहज व्यक्ति का किसी के प्रति द्वेष या
ईर्ष्या भाव देखा ही नहीं गया-‘यो न द्वेष्टि न कांक्षति च तस्य
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता’ (गीता)।
वह सबका मित्र है। उसकी दृष्टि में सभी समान हैं। हम झुँझलाते हैं पर हमारे बैठे-बैठे ही कोई अदना-सा कवि, लेखक अपनी रचना उनके हाथों में, कक्ष का कपाटों को उद्घाटित कर, बड़ी सहजता से थमा जाता है और वह छपे या नहीं छपे, श्री अवस्थी उसे इस तरह हाथों से सँजो लेते हैं जैसे वह सामान्य रचना नहीं होकर ‘जूही की कली’ हो। यहीं हमें याद आती है गीता के समभाव की बात—समानता समदृष्टि ही योग है-‘समत्वं योग उच्यते।’ श्री अवस्थी को जिसने सही ढंग से पहचाना उसने उन्हें यारों का यार, ‘यार-बादशाह’ ही कहा। अवस्थी संवेदनशील, समदर्शी तथा ईर्ष्या-द्वेषरहित ऐसे व्यक्ति हैं जिनका विरोध कोई नहीं कर सकता।
उपनिषदकार ने कहा-‘आत्मा का विकास करो, उसे नहीं मारो वरना घोर अंधकार में प्रवेश करोगे।’
हिंदी जगत् में कोई व्यक्ति लगातार चालीस वर्षों तक संपादक रहा हो और वह भी एक प्रतिष्ठान का जिसे इतना सम्मान मिला हो, कोई नहीं है।
राजेन्द्र अवस्थी सधे और सुविख्यात संपादक रहे हैं, उन्होंने जिस पत्र-पत्रिका को हाथ में लिया है, आसमान में पहुँचा दिया। उनकी टिप्पणियाँ अत्यंत मूल्यवान हैं। उनका कहना है कि मैंने एक भी घटना न बनाकर लिखी है और न कभी झूठ-फरेब पत्रकारिता को स्वीकारा। जो जैसा है, जो सही है, जो जागृत है, उसी पर उन्होंने लिखा है। इस दृष्टि से यह कृति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वे ‘कादंबिनी’ में ‘आखिर कब तक ?’ स्तंभ निरंतर लिखते रहे हैं। यह पुस्तक इसी स्तंभ की अत्यंत सजग और सत्य टिप्पणियों के अंश हैं।
राजेन्द्र अवस्थी कथाकार और पत्रकार तो हैं ही, उन्होंने सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामयिक विषयों पर भी भरपूर लिखा है। अनेक दैनिक-समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं में उनके लेख धड़ल्ले से छपते रहे। उनकी तीखी टिप्पणियाँ अनेक बार आक्रोश और विवाद को भी जन्म देती रही हैं, लेकिन अवस्थी जी कभी भी अपनी बात कहने से नहीं चूकते। वह कहेंगे और बहुत निडर तथा बेबाक होकर कहेंगे, भले ही उनके मित्र भी उनसे अप्रसन्न क्यों न हो जाएँ। उनका यह लेखन समसामयिक साहित्य का दस्तावेज बन गया। उन्होंने कई बड़े लोगों के जीवन को आधार बनाकर औपन्यासिक कृतियाँ दी हैं और उनमें उनकी विशेषताओं के साथ ही दुर्बलताओं की भी चर्चा की है। आखिर बड़ी-बड़ी हस्तियों से उनका साबका तो पड़ता ही रहा। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि बहुत बड़े लोगों के वह आत्मीय रहे हैं। ऐसे लेखन से उनका क्षेत्र व्यापक बना और साहित्य के घेरे के बाहर भी अन्य क्षेत्रों में उनकी खासी पहचान बन पाई।
अवस्थी जी अकसर कहते हैं ‘मैं देवता नहीं, आदमी हूँ।’ इन शब्दों के परिवेश में उनके जीवन का पूरा चित्र उभरता है। अच्छाइयों और दुर्बलताओं का सम्मिश्रण-सा एक व्यक्तित्व जिसने कभी कुछ छिपाने का प्रयास नहीं किया और न जिसने ‘सवारों’ में अपनी गिनती कराने की चेष्टा की। असहज स्थितियों में भी सहज बने रहना जिसकी विशेषता रही।
यह ठीक ही कहा जाता है कि अवस्थी जी का जीवन एक खुली किताब है, जो कुछ है, सामने है। सत्य पर पर्दा डालने का प्रयास नहीं करना ही ‘अवस्थी’ कहलाना है। भूमिका में कहने को बहुत नहीं रह जाता। प्रायः सारी बातें संगृहीत लेखों में आ गई हैं। इस दृष्टि से ‘आखिर कब तक ?’ हिंदी साहित्य की अन्यतम और निर्विवाद सत्य से भरपूर अमर कृति सिद्ध होगी।
वह सबका मित्र है। उसकी दृष्टि में सभी समान हैं। हम झुँझलाते हैं पर हमारे बैठे-बैठे ही कोई अदना-सा कवि, लेखक अपनी रचना उनके हाथों में, कक्ष का कपाटों को उद्घाटित कर, बड़ी सहजता से थमा जाता है और वह छपे या नहीं छपे, श्री अवस्थी उसे इस तरह हाथों से सँजो लेते हैं जैसे वह सामान्य रचना नहीं होकर ‘जूही की कली’ हो। यहीं हमें याद आती है गीता के समभाव की बात—समानता समदृष्टि ही योग है-‘समत्वं योग उच्यते।’ श्री अवस्थी को जिसने सही ढंग से पहचाना उसने उन्हें यारों का यार, ‘यार-बादशाह’ ही कहा। अवस्थी संवेदनशील, समदर्शी तथा ईर्ष्या-द्वेषरहित ऐसे व्यक्ति हैं जिनका विरोध कोई नहीं कर सकता।
उपनिषदकार ने कहा-‘आत्मा का विकास करो, उसे नहीं मारो वरना घोर अंधकार में प्रवेश करोगे।’
हिंदी जगत् में कोई व्यक्ति लगातार चालीस वर्षों तक संपादक रहा हो और वह भी एक प्रतिष्ठान का जिसे इतना सम्मान मिला हो, कोई नहीं है।
राजेन्द्र अवस्थी सधे और सुविख्यात संपादक रहे हैं, उन्होंने जिस पत्र-पत्रिका को हाथ में लिया है, आसमान में पहुँचा दिया। उनकी टिप्पणियाँ अत्यंत मूल्यवान हैं। उनका कहना है कि मैंने एक भी घटना न बनाकर लिखी है और न कभी झूठ-फरेब पत्रकारिता को स्वीकारा। जो जैसा है, जो सही है, जो जागृत है, उसी पर उन्होंने लिखा है। इस दृष्टि से यह कृति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वे ‘कादंबिनी’ में ‘आखिर कब तक ?’ स्तंभ निरंतर लिखते रहे हैं। यह पुस्तक इसी स्तंभ की अत्यंत सजग और सत्य टिप्पणियों के अंश हैं।
राजेन्द्र अवस्थी कथाकार और पत्रकार तो हैं ही, उन्होंने सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामयिक विषयों पर भी भरपूर लिखा है। अनेक दैनिक-समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं में उनके लेख धड़ल्ले से छपते रहे। उनकी तीखी टिप्पणियाँ अनेक बार आक्रोश और विवाद को भी जन्म देती रही हैं, लेकिन अवस्थी जी कभी भी अपनी बात कहने से नहीं चूकते। वह कहेंगे और बहुत निडर तथा बेबाक होकर कहेंगे, भले ही उनके मित्र भी उनसे अप्रसन्न क्यों न हो जाएँ। उनका यह लेखन समसामयिक साहित्य का दस्तावेज बन गया। उन्होंने कई बड़े लोगों के जीवन को आधार बनाकर औपन्यासिक कृतियाँ दी हैं और उनमें उनकी विशेषताओं के साथ ही दुर्बलताओं की भी चर्चा की है। आखिर बड़ी-बड़ी हस्तियों से उनका साबका तो पड़ता ही रहा। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि बहुत बड़े लोगों के वह आत्मीय रहे हैं। ऐसे लेखन से उनका क्षेत्र व्यापक बना और साहित्य के घेरे के बाहर भी अन्य क्षेत्रों में उनकी खासी पहचान बन पाई।
अवस्थी जी अकसर कहते हैं ‘मैं देवता नहीं, आदमी हूँ।’ इन शब्दों के परिवेश में उनके जीवन का पूरा चित्र उभरता है। अच्छाइयों और दुर्बलताओं का सम्मिश्रण-सा एक व्यक्तित्व जिसने कभी कुछ छिपाने का प्रयास नहीं किया और न जिसने ‘सवारों’ में अपनी गिनती कराने की चेष्टा की। असहज स्थितियों में भी सहज बने रहना जिसकी विशेषता रही।
यह ठीक ही कहा जाता है कि अवस्थी जी का जीवन एक खुली किताब है, जो कुछ है, सामने है। सत्य पर पर्दा डालने का प्रयास नहीं करना ही ‘अवस्थी’ कहलाना है। भूमिका में कहने को बहुत नहीं रह जाता। प्रायः सारी बातें संगृहीत लेखों में आ गई हैं। इस दृष्टि से ‘आखिर कब तक ?’ हिंदी साहित्य की अन्यतम और निर्विवाद सत्य से भरपूर अमर कृति सिद्ध होगी।
चाय वाला भी लेखक हो सकता है
जब मैं मुम्बई में था तो मुझे महाराष्ट्र के
कई गाँव, जिले और शहर देखने
को मिले थे। वहाँ फैली जिंदगी का नक्शा भी मैंने बारीकी से देखा था। सीधे
और सहज ढंग से रहने वाले महाराष्ट्र के स्त्री-पुरुष या लड़के-लड़कियाँ उस
शान-शौकत से कम ही रहते हैं, जो दिल्ली जैसे राजधानी शहर में दिखाई देती
है। कुछ लोगों को भ्रम है कि सारा फैशन मुंबई में है। यह मात्र भ्रम है यह
भ्रम मुंबई के फिल्मी स्टूडियों के अंदर ही देखने को मिलता है। उसके बाहर
सड़कों पर या बस स्टैंडों पर देखिए तो सफेद सूती साड़ी में अच्छी-से-अच्छी
पढ़ी लिखी लड़कियों को देखा जा सकता है। वहाँ के कॉलेजों और
विश्वविद्यालयों में भी दिल्ली जैसी तड़क-भड़क नहीं है। मुंबई और
महाराष्ट्र के लोग लाखों रुपयों का सौदा बिना लिखी-पढ़ी के करते हैं और
यदि वह पूरा नहीं हुआ तो ही ईमानदारी से वे पैसा वापस भी कर देते हैं।
मुंबई को बदनाम करके रखा है बॉलीवुड की दुनिया ने अथवा उस दुनिया के साथ
गहरा संपर्क जोड़ने वालों ने। उसकी अपनी कहनी है, जो फैशन से लेकर
देह-धर्म तक पहुँचती है। महाराष्ट्र की याद अचानक मुझे दिल्ली में इसलिए
आई कि यहाँ के कुछ छोटे पत्रों में मैंने एक व्यक्ति की कहानी पढ़ी है, जो
महाराष्ट्र के अमरावती जिले के छोटे-से गाँव तड़गाँव दशासर का है। उसका
जन्म राव परिवार में हुआ और अब दिल्ली में भी उसे लक्ष्मण राव के नाम से
जाना जाता है। सब कुछ हो जाए तो उसका पूरा नाम है लक्ष्मण राव चाय वाला।
विष्णु दिगंबर मार्ग पर स्थित हिंदी भवन के सामने वह बैठता है और छोटी-सी
दुकान चलाता है। सामने बैठने के लिए टेबल-कुर्सी जैसी चीजें नहीं हैं तो
लोग खड़े-खड़े या आसपास जमीन पर बैठकर ही उससे चाय खरीदते हैं और पी लेते
हैं। वह सुबह चाय की दुकान खोलता है और शाम को अपनी पूरी दुकान समेटकर
अपने घर चला जाता है। उसके पास साइकिल है और उसी साइकिल पर वह अपना सारा
सामान लाद देता है।
लक्ष्मण राव की कहानी मजेदार है। अवरावती में उसने मैट्रिक पास की, फिर एक मिल में काम करने लगा। कुछ दिनों के बाद मिल बंद हो गई, तब बिना किसी को बताए वह भोपाल आ गया। उस समय उसके पास चालीस रुपए थे और वह एक इमारत में मजदूरी का काम करता था। 1975 में वह दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसने कुछ काम ढूँढ़ना चाहा। जब काम नहीं मिला तो 1977 में पान बेचने की एक छोटी-सी दुकान लगा ली। यह दुकान इसी विष्णु दिगंबर मार्ग पर थी। धीरे-धीरे उसने पैसा जमा किए और उस दुकान को बढ़ाकर वहीं उसने चाय की दुकान लगा ली। इस व्यक्ति की चर्चा यहाँ–वहाँ अखबारों में इसलिए नहीं हुई कि उसने चाय की दुकान लगाई। उसकी चर्चा इसलिए हुई कि चाय की दुकान चलाते-चलाते उसने सोलह पुस्तकें लिख डालीं। इन पुस्तकों का उसने प्रकाशन भी करवा लिया। भारतीय अनुवाद परिषद ने लक्ष्मण राव का साहित्यिक जीवन बनाने में अच्छा योगदान दिया। बताया जाता है कि 27 मई, 1984 को उसे तीन मूर्ति में श्रीमती इंदिरा गाँधी से मिलने का अवसर मिला। बस, तभी से उसने पुस्तक लिखना शुरू किया। सुबह आठ बजे साइकिल के कैरियर पर अपनी पुस्तकों के बक्से को लेकर वह कई स्कूलों में जाता था और किसी तरह वहाँ अपनी पुस्तकें बेच लेता था।
पुस्तक लिखने के बारे में भी एक खासी घटना उसके जीवन में घटित हुई। वह जब सातवीं कक्षा में था तो उसके मित्र रामदास की अकस्मात् मृत्यु हो गई। वह उसका बहुत गहरा दोस्त था। तब उसे लेकर उसने स्वयं को समझने की कोशिश की और एक खासा पुरा उपन्यास लिख डाला। उसके अब तक सात उपन्यास, दो नाटक और कई किताबें छप चुकी हैं। उसका सही चेहरा तब सामने आया, जब उसका उपन्यास ‘नर्मदा’ एक समारोह में रिलीज हुआ। इसके पहले उसने ‘रामदास’ नाम से एक उपन्यास और लिखा था, जो वास्तव में उसके मित्र की कहानी है। लक्ष्मण राव अब एक लेखक है, लेकिन चाय बनाने में इतना सिद्धहस्त है कि वह अपना धंधा नहीं छोड़ना चाहता। कुछ लोग उससे मिले भी और तब उससे पूछा कि आखिर अब भी चाय की दुकान क्यों लगा रखी है ? तब उसने कहा कि चाय की दुकान लगाकर भी लेखक बना जा सकता है। यह सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि जिस असुरक्षा के माहौल में वह रहता है, उससे उसे एक ऐसा उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली कि आतंकवाद की गहराइयों को भी वह भली भाँति समझ गया। जो भी हो, आज भी महाराष्ट्र का लक्ष्मण राव हिंदी भवन के सामने बैठकर चाय की दुकान चलाता है और लेखन-कार्य भी करता है। इससे पता चलता है कि लेखक बनने के लिए कोई बड़ा पद चाहिए या बड़ी जगह। उसका मस्तिष्क सबसे बड़ा है।
लक्ष्मण राव की कहानी मजेदार है। अवरावती में उसने मैट्रिक पास की, फिर एक मिल में काम करने लगा। कुछ दिनों के बाद मिल बंद हो गई, तब बिना किसी को बताए वह भोपाल आ गया। उस समय उसके पास चालीस रुपए थे और वह एक इमारत में मजदूरी का काम करता था। 1975 में वह दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसने कुछ काम ढूँढ़ना चाहा। जब काम नहीं मिला तो 1977 में पान बेचने की एक छोटी-सी दुकान लगा ली। यह दुकान इसी विष्णु दिगंबर मार्ग पर थी। धीरे-धीरे उसने पैसा जमा किए और उस दुकान को बढ़ाकर वहीं उसने चाय की दुकान लगा ली। इस व्यक्ति की चर्चा यहाँ–वहाँ अखबारों में इसलिए नहीं हुई कि उसने चाय की दुकान लगाई। उसकी चर्चा इसलिए हुई कि चाय की दुकान चलाते-चलाते उसने सोलह पुस्तकें लिख डालीं। इन पुस्तकों का उसने प्रकाशन भी करवा लिया। भारतीय अनुवाद परिषद ने लक्ष्मण राव का साहित्यिक जीवन बनाने में अच्छा योगदान दिया। बताया जाता है कि 27 मई, 1984 को उसे तीन मूर्ति में श्रीमती इंदिरा गाँधी से मिलने का अवसर मिला। बस, तभी से उसने पुस्तक लिखना शुरू किया। सुबह आठ बजे साइकिल के कैरियर पर अपनी पुस्तकों के बक्से को लेकर वह कई स्कूलों में जाता था और किसी तरह वहाँ अपनी पुस्तकें बेच लेता था।
पुस्तक लिखने के बारे में भी एक खासी घटना उसके जीवन में घटित हुई। वह जब सातवीं कक्षा में था तो उसके मित्र रामदास की अकस्मात् मृत्यु हो गई। वह उसका बहुत गहरा दोस्त था। तब उसे लेकर उसने स्वयं को समझने की कोशिश की और एक खासा पुरा उपन्यास लिख डाला। उसके अब तक सात उपन्यास, दो नाटक और कई किताबें छप चुकी हैं। उसका सही चेहरा तब सामने आया, जब उसका उपन्यास ‘नर्मदा’ एक समारोह में रिलीज हुआ। इसके पहले उसने ‘रामदास’ नाम से एक उपन्यास और लिखा था, जो वास्तव में उसके मित्र की कहानी है। लक्ष्मण राव अब एक लेखक है, लेकिन चाय बनाने में इतना सिद्धहस्त है कि वह अपना धंधा नहीं छोड़ना चाहता। कुछ लोग उससे मिले भी और तब उससे पूछा कि आखिर अब भी चाय की दुकान क्यों लगा रखी है ? तब उसने कहा कि चाय की दुकान लगाकर भी लेखक बना जा सकता है। यह सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि जिस असुरक्षा के माहौल में वह रहता है, उससे उसे एक ऐसा उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली कि आतंकवाद की गहराइयों को भी वह भली भाँति समझ गया। जो भी हो, आज भी महाराष्ट्र का लक्ष्मण राव हिंदी भवन के सामने बैठकर चाय की दुकान चलाता है और लेखन-कार्य भी करता है। इससे पता चलता है कि लेखक बनने के लिए कोई बड़ा पद चाहिए या बड़ी जगह। उसका मस्तिष्क सबसे बड़ा है।
मुंबई मुंबई है, दिल्ली दिल्ली है !
कई वर्ष पुरानी बात है। तब मैं मुंबई में था।
मुंबई की शामों का अपना मजा
होता है। ऐसी शामें और कहीं देखना मुश्किल है। मुझे सैटू विंसटर की शामें
अकसर याद आती हैं। मरीन ड्राइव के पास एक छोटे-से फ्लैट में मोहन राकेश
रहा करते थे। प्रायः हमारे साथ कृष्ण चंदर, राजेन्द्र सिंह बेदी, राज
बेदी, गंगाधर गाडगिल और धर्मवीर भारती हुआ करते थे। सारे दिन की थकान और
दुःख दर्द को मिटाने के लिए हमारे मित्र रामरिख मनहर वह काम किया करते थे,
जो उस समय की मुंबई में और किसी के वश का नहीं था। वह अकसर ओपेरा हाउस
जाया करते थे और एक अच्छे चुस्त-दुरुस्त दोस्त के नाते सामग्री हमारे
सामने लाकर रख देते थे। उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू होता था।
राजेन्द्र सिंह बेदी की नाक में ऐसी अजीब-सी सुगन्ध थी कि हम सब अपनी हार
मान लेते थे। कई बार उन्होंने रामरिख मनहर को वापस ओपेरा हाउस भेजा था और
कहा था कि माल लाया करो तो ठीक लाया करो। बेचारे रामरिख मनहर बिना किसी
गिला-शिकवा के हमारी फरमाइशें पूरी कर देते थे। इसके बाद गपबाजी का
सिलसिला शुरू होता। उसमें उन दिनों ‘टाइम्स ऑफ
इंडिया’ के जनरल मैनेजर जे.सी. जैन से लेकर ताजी से ताजी आने
वाली फिल्मी अभिनेत्रियों की बातें हुआ करती थीं। जे.सी. जैन को कभी किसी
ने फोन पर सुना होतो उन्हें याद होगा कि उनकी पहचान (वे अब भले ही नहीं
रहे) ठेठ लड़कियों जैसी महीन आवाज से बनी। रौब-दाब यह कि एक दिन उन्होंने
मुझे ‘गेट वे ऑफ इंडिया’ से कुलाबा पैदल जाते देख
लिया। उस समय तो वे अपनी कार लेकर निकल गए, लेकिन अगले दिन साढ़े नौ बजे,
जो हमारी कॉफी का समय हुआ करता था, उन्होंने बुलाकर कहा,
‘‘कल आप कुलाबा की तरफ जा रहे
थे।’’ मैं जानता हूँ, यह पूछने का अर्थ क्या है।
मैंने कहा, ‘‘जी हाँ। वहाँ के सिनेमाघर का मालिक मेरा
दोस्त है, उसके पास तक जा रहा था।’’ जैन साहब ने
तुरन्त उत्तर दिया, ‘‘भाई, मैं यह नहीं पूछ रहा कि आप
कहाँ जा रहे थे। मैं तो कहना यह चाहता हूँ कि आप ‘टाइम्स ऑफ
इंडिया’ में एडिटर हैं, फिर आपको पैदल बिलकुल नहीं चलना चाहिए।
टैक्सी में जाइए और बिल कंपनी के नाम बना लीजिए।’’ यह
बात जब मैंने अपने दोस्तों को बताई तो सचमुच वे सब जैन साहब पर बेहद
कृपालु हो गए थे। यहाँ तक कि एक दिन हम लोगों ने उन्हें सैटू विंसटर में
बुलाया भी था। वहाँ क्या हुआ, यह सब बताना व्यर्थ है। बात उस समय की थी,
हुई और हो गई। यह तो नाटक का एक हिस्सा था। इस तरह के वहाँ ढेर-से किस्से
हम रोज ही तत्काल तैयार करते थे। उसमें सबसे ज्यादा परेशान धर्मवीर भारती
हुआ करते थे, क्योंकि वे अपने साथ पुष्पा को भी लेकर आया करते थे।
पुष्पाजी को चिढ़ाने में हमने कभी कमी नहीं की। कृष्ण चंदर ठेठ रूस के
हाथों बिके हुए आदमी थे। मेरा खयाल है कि सबसे ज्यादा पुस्तकें उनकी ही
छपीं और सारी पुस्तकों के अनुवाद रूसी में हुए और इसलिए हर महीने उन्हें
खासा पैसा रूस से मिलता था। वैसे भी कृष्ण चंदर खुशकिस्मत आदमी थे। उनकी
पत्नी और बच्चे उनसे बहुत दूर अँधेरी में रहा करते थे। कृष्ण चंदर के साथ
रहती थीं—सलमा सिद्दीकी। सलमा बेहद खूबसूरत तो थीं ही, लिखती भी
अच्छा थीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन की
भतीजी भी थीं। सलमा में पूरा मुगालिया ठाठ और नफ्फासी भरी हुई थी, इसलिए
कई बार तो उनके हाथ का खाना खाने के लिए भी हम लोग बांद्रा जाया करते थे,
जहाँ कृष्ण चंदर का घर था। मुझे याद है, उनके हाथ का राजमा मैंने जो खाया
था, जिंदगी में आज तक खाने को नहीं मिला, इसलिए मैंने अब राजमा खाना बन्द
कर दिया। राजेन्द्र सिंह बेदी की दूसरी खासियत थी कि वे सारे जोक सरदारों
पर ही सुनाया करते थे और सरदार होते हुए भी ठाठ से सिगरेट पीते थे। राकेश
अपने अट्टहास के लिए प्रसिद्ध थे। कहीं भी हों, घर हो या होटल का कोना,
जहाँ राकेश बैठे होंगे, बिना अट्टहास किए नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर मुंबई
की हमारी हर शाम अब एक सुनहरा सपना बनकर रह गई है।
एक बात हम लोग अकसर रोज किया करते थे कि मुंबई कभी बदलेगी भी या नहीं ? उत्तर साफ था कि मुंबई शहर को समंदर ने चारों तरफ से बाँध कर रखा है। न तो मुंबई की कोई सड़क बदल सकती है और न लोकल ट्रेनों का बिछाया हुआ जाल बदलेगा। मुंबई मुंबई रहेगी। वहाँ की बोली का जो अंदाज है, वह हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। मराठी और हिंदी का मुंबइया संस्करण केवल मुंबई की बपौती है।
एक बात हम लोग अकसर रोज किया करते थे कि मुंबई कभी बदलेगी भी या नहीं ? उत्तर साफ था कि मुंबई शहर को समंदर ने चारों तरफ से बाँध कर रखा है। न तो मुंबई की कोई सड़क बदल सकती है और न लोकल ट्रेनों का बिछाया हुआ जाल बदलेगा। मुंबई मुंबई रहेगी। वहाँ की बोली का जो अंदाज है, वह हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। मराठी और हिंदी का मुंबइया संस्करण केवल मुंबई की बपौती है।
जी हाँ, और दिल्ली दिल्ली है !
जब मैं दिल्ली आया था तो मुझे लग रहा था कि
मैं देहात में आ गया
हूँ—न वैसी शामें, न भाग-दौड़ और न मुंबई जैसे चटकारे। दिल्ली
आपस की लड़ाई में मुसलमानों की कृपा से मारी जाती रही। यहाँ के अधिकांश
लोग विभाजन के बाद रावलपिंडी, पेशावर और कराची से आकर बस गए और वहाँ की बू
आज तक नहीं गई। मैं 1964 में दिल्ली आया था और बड़े शहरों में इससे ज्यादा
गंदा शहर मुझे कोई और देखने को नहीं मिला। कोई नई बात नहीं कि एक बार कोई
रास्ता देख लें तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता। अब पिछले दो-चार वर्षों से
दिल्ली का नक्शा बदल रहा है। वैसे तो अभी भी आधी दिल्ली खुदी पड़ी है और
कूड़े-कचरे के ढेरों की जगह-जगह कमी नहीं है। मुंबई की तरफ झोपड़ियाँ उतनी
ज्यादा भले न हों लेकिन यहाँ भी जो झुग्गी-बस्तियाँ हैं, वे अपराध का सबसे
बड़ा केंद्र हैं। तमिलनाडु के भूखे लोगों ने यहाँ अड्डा जमाकर रखा है और
हर घर में काम करने वाला, चाहे लड़का हो या लड़की, वह तमिलनाडु का ही होता
है। उनका अपना काम करने का सलीका है और अपने रहने का ढंग।
दिल्ली जैसी भी हो लेकिन है तो आखिर इस महान् देश की राजधानी। लेकिन इस राजधानी में धीरे-धीरे विदेशों की नकल इस तेजी से की जा रही है जैसे रोसकोर्स के घोड़े दौड़ते हैं। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक तीन-चौथाई दिल्ली खुदी पड़ी है। बड़े-बड़े खंभे लगे हुए हैं और कल्पना की जा रही है कि जमीन से बहुत ऊपर जापान की तरह यहाँ भी रेलें चलेंगी। दिल्ली के लिए यह जरूरी है क्योंकि इसके किनारे समुद्र नहीं है। समुद्र नहीं है तो पूरा शहर मकड़ी के जाले-सा फैला हुआ है। चारों दिशाओं में चले जाइए, दिल्ली का अंत नहीं है। इस दिल्ली में अनंत गाँव भी हैं और मजे की बात तो यह है कि उन मुहल्लों के नाम अब भी उन गाँवों के नामों पर ही चलते हैं—खिचड़ीपुर, मंगोलपुरी, सैयदनगर, भोगल इत्यादि। मुझे आश्चर्य तब होता है, जब बसों के पीछे इन गाँवों के नाम लिखे होते हैं और हम ठाठ से कहते हैं कि हम देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग जरूर आश्चर्य में होगें कि वे दिल्ली में ही जा रहे हैं कि उस गाँव में जा रहे हैं।
जब मैं आया था तो मैंने सोचा था कि दिल्ली कभी नहीं बदलेगी, लेकिन अब हालत यह है कि दिल्ली इस तरह बदल रही है कि यदि किसी सड़क या किसी चौराहे से आप दो-चार दिन न निकलें तो उसके बाद जब वहाँ से जाएँगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह वही जगह है, जहाँ से आप अकसर आते-जाते रहे हैं। यहाँ के नेताओं ने सड़कों को दो भागों में बाँट दिया है। इस शहर में इस तरह तलाक हो गया है कि एक भूली हुई जगह से दोबारा पहुँचना है तो इतना बड़ा चक्कर लगाना होगा—जैसे आप फिर से शादी करने के लिए जा रहे हों। वैसे भी मैंने सुना है, दिल्ली में आजकल तलाक और शादी दोनों साथ-साथ धड़ल्ले से चल रहे हैं। यहाँ कि पढ़ी-लिखी लड़कियाँ मुंबई की उन लड़कियों की बराबरी करती हैं, जो स्टूडियो के भीतर सजी-सँवरी होती हैं। मुंबई में आम तौर पर सड़क पर लड़कियों को देख लीजिए, बहुत सीधी, सहज और सरल नजर आएँगी। दिल्ली की लड़कियों को यह सहजता पसंद नहीं है। वे तो फैशन शो और स्टूडियों में एक्टिंग करने वाली लड़कियों के भी कान काट रही हैं।
मैं एक बात और सोचता हूँ कि थोड़े दिनों में जब टोकियो और जापान के अन्य शहरों की तरह यहाँ आसमान में रेलें दौड़ने लगेंगी तो क्या हाल होगा ? इनके प्लेटफॉर्म ऊपर बनाए जाएँगे तो उनसे कितनी दुर्घटनाएँ होंगी ? यदि आधुनिक एक्सीलेटर लगाए जाएँगे तो उनमें फँसकर मरने वालों की संख्याओं को अखबारों में पढ़ना पड़ेगा। एक बात और मेरे दिमाग में आती है। जापान में दो तरह की हवाई ट्रेनें चलती हैं। एक तो सीधी-सादी, चुप और तेज भागती हुई और दूसरी थंडर ट्रेन। जब थंडर ट्रेन जापान में चलती है तो डिब्बे के भीतर आवाज नहीं होती लेकिन बाहर इतनी तेज आवाज करते हुए जाती है कि प्लेटफार्म भी काँपते हैं और आसपास के लोग भी काँप उठते हैं। इसका एक कारण है। मैंने तो सारी दुनिया देखी है, इतना तो बहुत दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि जापान से ज्यादा शांति दुनिया में कहीं नहीं है। वहाँ के लोग भी शांत नहीं है बल्कि वहाँ की हवा, वहाँ का आकाश, वहाँ की धरती, सब में अपार शांति विराजमान है। यह शायद परमाणु बम के हमले के बाद की प्रतिक्रिया है कि सारे लोग इतने डरे और सहमें हैं कि वे एकदम शांत हो गए। यहाँ तक कि नागासाकी और हिरोशिमा दोनों शहर तथा वहाँ के बगीचे, सड़कें एकदम शांत हैं। इन शहरों ने परमाणु बम का सबसे भयंकर संहारक रूप देखा है। दिल्ली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है इसलिए दिल्ली वालों को चिल्लाना, लड़ना, जोर से बोलना और छोटी-छोटी बातों में कत्ल कर देने की आदत पड़ गई है। निश्चय ही ऐसी स्थिति में दिल्ली में थंडर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती। जो ट्रेन चलेगी, वह भी भीड़ से भरी होगी और आवाज की कवायदें इतनी ज्यादा होंगी कि हर आदमी सोचेगा कि कब अपनी जगह पहुँच जाएँ और इनसे दूर चले जाएँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं आया था, तब मैंने दिल्ली को देहात कहा था, अब मजबूर होकर दिल्ली को बाजार कहना पड़ेगा।
दिल्ली जैसी भी हो लेकिन है तो आखिर इस महान् देश की राजधानी। लेकिन इस राजधानी में धीरे-धीरे विदेशों की नकल इस तेजी से की जा रही है जैसे रोसकोर्स के घोड़े दौड़ते हैं। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक तीन-चौथाई दिल्ली खुदी पड़ी है। बड़े-बड़े खंभे लगे हुए हैं और कल्पना की जा रही है कि जमीन से बहुत ऊपर जापान की तरह यहाँ भी रेलें चलेंगी। दिल्ली के लिए यह जरूरी है क्योंकि इसके किनारे समुद्र नहीं है। समुद्र नहीं है तो पूरा शहर मकड़ी के जाले-सा फैला हुआ है। चारों दिशाओं में चले जाइए, दिल्ली का अंत नहीं है। इस दिल्ली में अनंत गाँव भी हैं और मजे की बात तो यह है कि उन मुहल्लों के नाम अब भी उन गाँवों के नामों पर ही चलते हैं—खिचड़ीपुर, मंगोलपुरी, सैयदनगर, भोगल इत्यादि। मुझे आश्चर्य तब होता है, जब बसों के पीछे इन गाँवों के नाम लिखे होते हैं और हम ठाठ से कहते हैं कि हम देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग जरूर आश्चर्य में होगें कि वे दिल्ली में ही जा रहे हैं कि उस गाँव में जा रहे हैं।
जब मैं आया था तो मैंने सोचा था कि दिल्ली कभी नहीं बदलेगी, लेकिन अब हालत यह है कि दिल्ली इस तरह बदल रही है कि यदि किसी सड़क या किसी चौराहे से आप दो-चार दिन न निकलें तो उसके बाद जब वहाँ से जाएँगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह वही जगह है, जहाँ से आप अकसर आते-जाते रहे हैं। यहाँ के नेताओं ने सड़कों को दो भागों में बाँट दिया है। इस शहर में इस तरह तलाक हो गया है कि एक भूली हुई जगह से दोबारा पहुँचना है तो इतना बड़ा चक्कर लगाना होगा—जैसे आप फिर से शादी करने के लिए जा रहे हों। वैसे भी मैंने सुना है, दिल्ली में आजकल तलाक और शादी दोनों साथ-साथ धड़ल्ले से चल रहे हैं। यहाँ कि पढ़ी-लिखी लड़कियाँ मुंबई की उन लड़कियों की बराबरी करती हैं, जो स्टूडियो के भीतर सजी-सँवरी होती हैं। मुंबई में आम तौर पर सड़क पर लड़कियों को देख लीजिए, बहुत सीधी, सहज और सरल नजर आएँगी। दिल्ली की लड़कियों को यह सहजता पसंद नहीं है। वे तो फैशन शो और स्टूडियों में एक्टिंग करने वाली लड़कियों के भी कान काट रही हैं।
मैं एक बात और सोचता हूँ कि थोड़े दिनों में जब टोकियो और जापान के अन्य शहरों की तरह यहाँ आसमान में रेलें दौड़ने लगेंगी तो क्या हाल होगा ? इनके प्लेटफॉर्म ऊपर बनाए जाएँगे तो उनसे कितनी दुर्घटनाएँ होंगी ? यदि आधुनिक एक्सीलेटर लगाए जाएँगे तो उनमें फँसकर मरने वालों की संख्याओं को अखबारों में पढ़ना पड़ेगा। एक बात और मेरे दिमाग में आती है। जापान में दो तरह की हवाई ट्रेनें चलती हैं। एक तो सीधी-सादी, चुप और तेज भागती हुई और दूसरी थंडर ट्रेन। जब थंडर ट्रेन जापान में चलती है तो डिब्बे के भीतर आवाज नहीं होती लेकिन बाहर इतनी तेज आवाज करते हुए जाती है कि प्लेटफार्म भी काँपते हैं और आसपास के लोग भी काँप उठते हैं। इसका एक कारण है। मैंने तो सारी दुनिया देखी है, इतना तो बहुत दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि जापान से ज्यादा शांति दुनिया में कहीं नहीं है। वहाँ के लोग भी शांत नहीं है बल्कि वहाँ की हवा, वहाँ का आकाश, वहाँ की धरती, सब में अपार शांति विराजमान है। यह शायद परमाणु बम के हमले के बाद की प्रतिक्रिया है कि सारे लोग इतने डरे और सहमें हैं कि वे एकदम शांत हो गए। यहाँ तक कि नागासाकी और हिरोशिमा दोनों शहर तथा वहाँ के बगीचे, सड़कें एकदम शांत हैं। इन शहरों ने परमाणु बम का सबसे भयंकर संहारक रूप देखा है। दिल्ली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है इसलिए दिल्ली वालों को चिल्लाना, लड़ना, जोर से बोलना और छोटी-छोटी बातों में कत्ल कर देने की आदत पड़ गई है। निश्चय ही ऐसी स्थिति में दिल्ली में थंडर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती। जो ट्रेन चलेगी, वह भी भीड़ से भरी होगी और आवाज की कवायदें इतनी ज्यादा होंगी कि हर आदमी सोचेगा कि कब अपनी जगह पहुँच जाएँ और इनसे दूर चले जाएँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं आया था, तब मैंने दिल्ली को देहात कहा था, अब मजबूर होकर दिल्ली को बाजार कहना पड़ेगा।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book