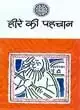|
सामाजिक >> निशिकान्त निशिकान्तविष्णु प्रभाकर
|
64 पाठक हैं |
||||||
निशिकान्त का कथाक्षेत्र 1920 से 1939 तक फैला हुआ है। यह यथार्थ हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम का प्रखर संक्रान्ति काल रहा है।
निशिकान्त विष्णुजी का पहला उपन्यास है। आमतौर पर साहित्यिक धारणा यही है
किसी साहित्यकार की पहली कृति अपने व्यक्तिगत जीवन-संघर्षों के अनुभवजन्य
यथार्थ का प्रामाणिक आकलन होती है। निशिकान्त का कथाक्षेत्र 1920 से 1939
तक फैला हुआ है। यह यथार्थ हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम का प्रखर
संक्रान्ति काल रहा है। इसका प्रतिबिम्ब हमारे सामाजिक और
सांस्कृतिक जीवन पर भी बड़े निर्णायक रूप में झलका है। इसी
सामाजिक और राजनीतिक संक्रमण-काल का पात्र है
‘निशिकान्त’।-वह सरकारी नौकरी छोड़कर
स्वतंत्रता-संग्राम में कूदने की प्रबल इच्छा और आकांक्षा के बावजूद अपनी
आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ऐसा न कर पाने के लिए विवश है।
ऐसे ही एक युवक की इच्छा,आकांक्षा, छटपटाहट और विवशता है निशिकान्त। इस
प्रकार यह उपन्यास तत्कालीन निम्न मध्यम वर्गीय युवक के आत्मसंघर्ष की
गाथा है-पूरी समग्रता के साथ। इसीलिए कथ्य की दृष्टि से यह एक ऐसी
प्रामाणिक दस्तावेज है जो बदली हुई परिस्थितियों में भी उतनी ही सटीक और
सही दिखायी देती है।निशिकान्त विष्णु जी का संभवतः सर्वाधिक विवादास्पद
उपन्यास है। पंजाब के बी.ए.पाठ्यक्रम में लग जाने के बाद एक हिन्दू
सम्प्रदाय-विशेष ने इसके विरुद्ध एक व्यापक आन्दोलन चलाकर इसे पाठ्यक्रम
से निकलवा दिया था।
दो शब्द
‘निशिकान्त’ का रचनाकाल सन् 1948 और ’50 के
बीच फैला
हुआ है। इसका प्रथम प्रकाशन सन् 1951 में चेतना प्रकाशन लि०, हैदराबाद
(आन्ध्र प्रदेश) से हुआ था। तब इसका नाम था ‘ढलती
रात’। यह
नाम क्यों बदला गया इसका कोई विशेष कारण नहीं है, फिर भी चेतना प्रकाशन से
जब यह प्रकाशित हुआ तो कुछ समालोचकों और मित्रों के हाथ में जाकर ही रह
गया। बाज़ार में न आ सका। और चेतना प्रकाशन भी अनेक कारणों से बन्द हो
गया।
शकुन अच्छा नहीं हुआ। समीक्षकों ने भी इसका स्वागत जैसा कि सदा होता है वैसा ही किया। किसी ने निकृष्ट कहा तो किसी ने सर्वश्रेष्ठ। और भी बहुत-सी अनर्गल बातें इसके बारे में कही गईं। तब इसका दूसरा संस्करण सन् 1955 में आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली से हुआ तो यह फिर एक दूषित चक्र में फँस गया। प्रकाशक महोदय सम्भवतः अपने प्रभाव के कारण इसे पंजाब विश्वविद्यालय की बी० ए० की परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगवाने में सफल हो गये। पंजाब आर्य समाज का गढ़ रहा है। उसे इस उपन्यास की विषय वस्तु उसके सिद्धान्तो के विरुद्ध लगी। इसलिए इसका पाठ्य-पुस्तक में रहना उसके नेताओं को स्वीकार्य नहीं हो सकता था, नहीं हुआ। उन्होंने इसके विरुद्घ आन्दोलन छेड़ दिया।
इसे नियति का व्यंग्य ही कह सकते हैं कि मेरी सारी शिक्षा-दीक्षा आर्य समाज के वातावरण में ही हुई। बीस वर्ष तक मैं उसका सक्रिय सदस्य रहा। अब भी उसके सम्बन्ध में अधिकारपूर्वक लिखता रहता हूँ, प्रशंसा भी पाई है। लेकिन उस समय आर्य समाज ने मेरे विरुद्ध जिस प्रकार जेहाद छेड़ा उसका परिणाम यही हो सकता था कि यह पुस्तक पाठ्य-क्रम से निकाल दी जाती।
यह सब कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है, इस सबकी चर्चा यहाँ असंगत है। संगत इतना ही है कि इस उपन्यास का तीसरा संस्करण निकालने के बाद इसका प्रकाशन न हो सका। क्यों न हो सका, इसकी भी एक कहानी है। उसकी चर्चा भी अभी रहने दें। अब यह नये रूप में सामने आ रहा है, कथा वहीं है, मात्र यहां-वहां से कुछ तराश दी गयी है। इसकी कथा-वस्तु का क्षेत्र सन् 1920 से लेकर सितम्बर 1939 तक फैला हुआ है। संयुक्त पंजाब इसकी सीमा है लेकिन इसी कारण इसे क्षेत्रीय उपन्यास नहीं कहा जा सकता। इसमें उस युग के एक ऐसे युवक की कहानी है जो परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फँस जाता है। बाहर निकलने के लिए छटपटाता है लेकिन परिस्थितियाँ उसे इस प्रकार जकड़ लेती हैं कि वह चाहकर भी उनसे मुक्त नहीं हो पाता। वह चाहता है देश के स्वाधीनता-संग्राम में भाग लेना, लेकिन उसे करनी पड़ती है उसी सरकार की नौकरी, जिसने उसके देश को गुलामी की ज़ंजीरों से जकड़ा हुआ है। उसी संघर्ष का इस उपन्यास में चित्रण है, लेकिन वह मात्र राजनीतिक नहीं है। निशिकान्त सामाजिक स्तर पर भी संघर्ष करता है। इसलिए तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का, प्रकारान्तर से आर्य समाज का भी इसमें चित्रण हुआ है। लेखक आक्रामक नहीं है, वह मात्र अपनी शक्ति के अनुसार स्थितियों का चित्रण करता है। इस कारण यदि किसी को चोट पहुंचती है तो उसके लिए लेखक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कुछ आलोचकों ने ‘निशिकान्त’ को कायर कहा है, प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता भी है, लेकिन वस्तुतः वह अनेक कारणों से विवश है। वह उन्हीं विवश करने वाली परिस्थितियों से जूझता है। उसके भीतर गहरा द्वन्द्व जन्म लेता है और अन्ततः वह ऊपर ही उठता है।
लेखक के रूप में मैं इतना ही कह सकता हूँ। यह कैसा बन पड़ा है यह आलोचक और पाठक जानें। अब तक जैसा कि मैंने अनुभव किया है आलोचकों ने कम पर पाठकों ने इसे अधिक पसन्द किया है। यह इसलिए हुआ कि आलोचकों ने इसे कला की कसौटी पर कसा है और पाठकों ने इसे अपने आस-पास बिखरी कथा के रूप में पहचाना है। धर्म की सत्ता अपने विकृत रूप में मनुष्य को किस प्रकार पतन की ओर धकेलती है इसका यत्किंचित चित्रण इसमें हुआ है। काल की दृष्टि से यह पचास वर्ष पुराना हो सकता है, लेकिन कथा-वस्तु की दृष्टि से आज भी हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनसे निशिकान्त जूझा था।
मुझे इतना ही कहना है। मैं उन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ जो इसके सृजन और प्रकाशन का कारण बने !
शकुन अच्छा नहीं हुआ। समीक्षकों ने भी इसका स्वागत जैसा कि सदा होता है वैसा ही किया। किसी ने निकृष्ट कहा तो किसी ने सर्वश्रेष्ठ। और भी बहुत-सी अनर्गल बातें इसके बारे में कही गईं। तब इसका दूसरा संस्करण सन् 1955 में आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली से हुआ तो यह फिर एक दूषित चक्र में फँस गया। प्रकाशक महोदय सम्भवतः अपने प्रभाव के कारण इसे पंजाब विश्वविद्यालय की बी० ए० की परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगवाने में सफल हो गये। पंजाब आर्य समाज का गढ़ रहा है। उसे इस उपन्यास की विषय वस्तु उसके सिद्धान्तो के विरुद्ध लगी। इसलिए इसका पाठ्य-पुस्तक में रहना उसके नेताओं को स्वीकार्य नहीं हो सकता था, नहीं हुआ। उन्होंने इसके विरुद्घ आन्दोलन छेड़ दिया।
इसे नियति का व्यंग्य ही कह सकते हैं कि मेरी सारी शिक्षा-दीक्षा आर्य समाज के वातावरण में ही हुई। बीस वर्ष तक मैं उसका सक्रिय सदस्य रहा। अब भी उसके सम्बन्ध में अधिकारपूर्वक लिखता रहता हूँ, प्रशंसा भी पाई है। लेकिन उस समय आर्य समाज ने मेरे विरुद्ध जिस प्रकार जेहाद छेड़ा उसका परिणाम यही हो सकता था कि यह पुस्तक पाठ्य-क्रम से निकाल दी जाती।
यह सब कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है, इस सबकी चर्चा यहाँ असंगत है। संगत इतना ही है कि इस उपन्यास का तीसरा संस्करण निकालने के बाद इसका प्रकाशन न हो सका। क्यों न हो सका, इसकी भी एक कहानी है। उसकी चर्चा भी अभी रहने दें। अब यह नये रूप में सामने आ रहा है, कथा वहीं है, मात्र यहां-वहां से कुछ तराश दी गयी है। इसकी कथा-वस्तु का क्षेत्र सन् 1920 से लेकर सितम्बर 1939 तक फैला हुआ है। संयुक्त पंजाब इसकी सीमा है लेकिन इसी कारण इसे क्षेत्रीय उपन्यास नहीं कहा जा सकता। इसमें उस युग के एक ऐसे युवक की कहानी है जो परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फँस जाता है। बाहर निकलने के लिए छटपटाता है लेकिन परिस्थितियाँ उसे इस प्रकार जकड़ लेती हैं कि वह चाहकर भी उनसे मुक्त नहीं हो पाता। वह चाहता है देश के स्वाधीनता-संग्राम में भाग लेना, लेकिन उसे करनी पड़ती है उसी सरकार की नौकरी, जिसने उसके देश को गुलामी की ज़ंजीरों से जकड़ा हुआ है। उसी संघर्ष का इस उपन्यास में चित्रण है, लेकिन वह मात्र राजनीतिक नहीं है। निशिकान्त सामाजिक स्तर पर भी संघर्ष करता है। इसलिए तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का, प्रकारान्तर से आर्य समाज का भी इसमें चित्रण हुआ है। लेखक आक्रामक नहीं है, वह मात्र अपनी शक्ति के अनुसार स्थितियों का चित्रण करता है। इस कारण यदि किसी को चोट पहुंचती है तो उसके लिए लेखक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कुछ आलोचकों ने ‘निशिकान्त’ को कायर कहा है, प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता भी है, लेकिन वस्तुतः वह अनेक कारणों से विवश है। वह उन्हीं विवश करने वाली परिस्थितियों से जूझता है। उसके भीतर गहरा द्वन्द्व जन्म लेता है और अन्ततः वह ऊपर ही उठता है।
लेखक के रूप में मैं इतना ही कह सकता हूँ। यह कैसा बन पड़ा है यह आलोचक और पाठक जानें। अब तक जैसा कि मैंने अनुभव किया है आलोचकों ने कम पर पाठकों ने इसे अधिक पसन्द किया है। यह इसलिए हुआ कि आलोचकों ने इसे कला की कसौटी पर कसा है और पाठकों ने इसे अपने आस-पास बिखरी कथा के रूप में पहचाना है। धर्म की सत्ता अपने विकृत रूप में मनुष्य को किस प्रकार पतन की ओर धकेलती है इसका यत्किंचित चित्रण इसमें हुआ है। काल की दृष्टि से यह पचास वर्ष पुराना हो सकता है, लेकिन कथा-वस्तु की दृष्टि से आज भी हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनसे निशिकान्त जूझा था।
मुझे इतना ही कहना है। मैं उन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ जो इसके सृजन और प्रकाशन का कारण बने !
22-9-86
-विष्णु प्रभाकर
पहला खण्ड
1
वे बडी तेज़ी से चल रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि वे रामनाथ के घर के
पास आ गये हैं तभी एक करुण ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वे ठिठक गये। फिर
शान्त-स्थिर गति से बैठक में चले गये। निशिकान्त ने देखा, उस वर्गाकार
कमरे में घेरा बनाकर पाँच-छः मनुष्य सिर नीचा किये बैठे हैं। लालटेन के
प्रकाश में उनके विषादपूर्ण मुख और भी भयानक हो उठे हैं। उनके बीच में
बैठा रामनाथ सहसा हूक मारकर रो उठता है, ‘‘मेरे बच्चे
! मेरे
बेटे ! मैं क्या करूँ ?’’ और तब उन पुरुषों में से
कोई बोल
उठता था है, ‘‘सब्र करो रामनाथ, भगवान् की यही इच्छा
थी।’
भगवान का नाम सुनकर रामनाथ का दर्द और भी टीस उठा, ‘‘भगवान का मैंने क्या बिगाड़ा था ? उसने मेरे बेटे को मुझेसे क्यों छीना ?’’
उसी समय उसने निशिकान्त और पण्डितजी को देखा। वे दोनों चुपचाप एक कोने में जा बैठे थे। उन्हें देखकर रामनाथ और भी ज़ोर से रो उठा, ‘‘पण्डितजी, पण्डितजी ! मैं क्या करूँ ?’’
पण्डितजी ने दृढ़ स्वर में कहा, ‘‘तुम्हारा बेटा बहादुर था वह शहीद की मौत मरा है, उसके लिए रोते हो ?’’
निशिकान्त सान्त्वना के स्वर में बोला, ‘‘रामनाथ जी ! तुम्हारा दुःख बहुत बड़ा है, पर अब क्या हो सकता है ? तुम रोओगे तो तुम्हारे बच्चों को कौन सँभालेगा ? उनकी माँ भी तो नहीं है।’’
‘‘ठीक है कान्त भइया ! पर....पर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था ? ’’
पण्डितजी तड़प उठे, ‘‘भगवान् मेरा जाने, तुम्हें यही पता नहीं कि जो बिगाड़ने वाले होते हैं वे कभी सामने नहीं आते। वे कायर होते हैं।’’
वहाँ बैठे हुए आदमियों में से एक ने इस बात का समर्थन किया, ‘‘जी हाँ ! आप ठीक कहते हैं, उन्होंने घर के अन्दर से गोली चलाई।’’ दूसरे ने कहा, ‘‘यही तो। वे अन्दर थे और हिन्दू बाहर।’’
‘‘हिन्दू कायर हैं, नहीं तो.....’’
‘‘नहीं तो क्या ?’’ निशिकान्त एकाएक पूछ बैठा।
जिनसे पूछा गया था वह एक बार तो सकपका गये, पर फिर दृढ़ स्वर में बोले, ‘‘बाबूजी ! आपको क्या पता ? मैं जानता हूँ, हिन्दुओं ने रायबहादुर से कहा था, ‘‘एक बार अपनी बन्दूक दे दो, फिर हम देख लेंगे’, लेकिन रायबहादुर ! वह हिन्दू थे और हिन्दू होते हैं दयालु, अहिंसा के पुजारी। सो उसका फल उन्होंने भोगा। आप मरे और साथ में चार को और ले गये ।’’
‘‘हाँ, बेचारे चारों ही निर्दोष मारे गये। रामनाथ का लड़का स्कूल से लौट रहा था.....’’
‘‘चिम्मा कुम्हार के बेटे ने समझा था कि कोई तमाशा हो रहा है।’’
‘‘और लाला देवादीन तो खाना खाने घर जा रहे थे।’’
‘‘और बाबू मोहनकृष्ण ! वह बेचारा तो अपने घर में बैठा था।’’
‘‘बाबू मोहनकृष्ण,’’ निशिकान्त ने धीरे से कहा, ‘‘जो उन्हें जानते हैं वे किसी भी शर्त पर यह नहीं मान सकेंगे कि मोहनकृष्ण मुसलमानों से लड़ सकता है।’’
‘‘और उसी आदमी को मुसलमानों ने मार डाला।’’ रामनाथ ने आह भरकर कहा, ‘‘न जाने भगवान् क्या चाहते हैं ! मुझे ही देखो, मैंने जन्म-भर कांग्रेस की सेवा की है और मेरा बच्चा मुसलमानों के हाथों मारा गया। दुनिया क्या कहेगी ?’’
‘‘कहेगी क्या ?’’ पण्डितजी ने कहा, ‘‘और कहेगी भी तो तुम फिक्र क्यों करते हो। जो होना था, हो चुका। तुम मर नहीं सकते। और मरो भी क्यों ? जीओ और शान से जीओ।’’
और फिर उठते-उठते कहा, ‘‘रामनाथ, मैं कहता हूँ कि रोज सवेरे रामायण का पाठ किया करो। भगवान् मेरा जाने, रामायण से बढ़कर कोई पुस्तक इस संसार में नहीं है। राजनीति, धर्म और आचरण, सभी कुछ उसमें है। पढ़कर मन को शान्ति मिलती है और तुम्हारा जी न लगे तो मेरे पास आ जाया करो।’’
और वे विदा माँगकर बाहर आ गये। सड़क की बिजली जल चुकी थी और उसका गदराया हुआ प्रकाश अन्धकार के साथ गलबाहीं डाले इधर-उधर बिखरा पड़ा था। सन्नाटा ऐसा था कि कभी-कभी उन लोगों के अपने के अपने ही पदचाप उनके भय का कारण बन जाते थे। वे कुछ दूर तक चुपचाप बिना बोले चलते रहे।
फिर सहसा पण्डितजी बोल उठे, ‘‘देखा निशिकान्त ! यह हमारी सहानुभूति है। कितने आदमी थे इसके पास !’’
निशिकान्त ने कहा, ‘‘आदमी देखना चाहते हो तो रायबहादुर के घर चलो ।’’
रायबहादुर का नाम सुनते ही पण्डितजी को क्रोध आ गया। बोले, ‘‘मैं वहाँ नहीं जाऊँगा।’’
‘‘सोचता मैं भी यही हूँ।’’
पण्डितजी ने कहा, ‘‘हम कितने बेईमान हैं। रामनाथ कांग्रेस का कितना काम करता है ! नेता सजे-सजाये रंगमंच पर लैक्चर देकर चले जाते हैं, परन्तु सभा का प्रबन्ध करना और उसका संदेश घर-घर पहुँचाना इसी का काम है। यह इस भवन की नींव है, परन्तु इसीलिए आज इसके पास कोई नहीं है।’’
निशिकान्त उनकी ओर देखकर बोला, ‘‘पण्डितजी ! नींव आँखों से ओझल रहती है। उसके पास कोई नहीं जा सकता, लेकिन यही उसकी शक्ति है। सहानुभूति के अभाव में ही आदमी अपने पैरों खड़ा होना सीखता है।’’
पण्डितजी ने तलखी से जवाब दिया, ‘‘निशिकान्त ! यह सब बेईमानी है। मैं पूछता हूँ, आखिर क्यों सब लोग रायबहादुर के घर गये और रामनाथ के पास नहीं आये ?’’
निशिकान्त के मुँह से दीर्घ निश्वास निकल गया। ऊपर देखता हुआ वह धीरे से बोला, ‘‘पण्डितजी ! इस प्रश्न का उत्तर है। उत्तर सभी प्रश्नों का होता है, परन्तु केवल उत्तर से प्रश्न हल नहीं होता। हल उत्तर के विश्लेषण और फिर विश्लेषण के निष्कर्षों पर अमल करने से होता है।’’
‘‘तो ठीक है, मैं रायबहादुर के घर नहीं जाऊँगा। चिम्मा कुम्हार के घर चलो। ’’
‘‘चलिये ! लेकिन देर हो चली है। आठ बजे तक हमें घर पहुँच जाना चाहिए।’’
यह कहकर उसने फिर ऊपर देखा। सप्तर्षि-मण्डल मकानों के पीछे से उठकर ऊपर आ गया था और व्याध हरिणियों पर तीर साधे मंत्र की भांति आगे बढ़ रहा था। उसके मन में उठा, कितने शान्त और कितने सुन्दर हैं ये तारागण ! क्या इन्होंने कल होने वाले रक्त-पात को नहीं देखा ? क्या ये नहीं जानते कि रायबहादुर ने बन्दूक नहीं चलाई थी ?
पण्डितजी बोल उठे, ‘‘भाई, अब सबके घर नहीं जा सकते।’’
‘‘मैं भी यही सोचता हूँ।’’
‘‘एक स्थान पर और हो आते हैं। बाकी कल चलेंगे।’’
निशिकान्त ने क्षण-भर सोचकर कहा, ‘‘पण्डितजी, आज और कल में बड़ा अन्तर है।’’
‘‘तो ?’’
‘‘ऐसा करिये। आप चिम्पा के घर चले जाइये। मैं मोहनकृष्ण के घर जा रहा हूँ, वहाँ तो मुझे कल ही जाना चाहिए था।’’
‘‘मैं जानता हूँ, तुमने उसकी स्त्री को पढ़ाया है।’’
और फिर वे दोनों दो रास्तों पर मुड़ गये। तब तक चाँद निकल आया था और उसका धीमा पर शान्त प्रकाश धरती के विषाद को दूर करने के लिए धीरे-धीरे नीचे उतर रहा था। निशिकान्त का मन फिर अवसाद से भरने लगा। उससे बचने के लिए उसने तेजी से चलना शुरू किया; परन्तु दूसरे क्षण ही वह भयंकर वेग से काँप उठा। किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। देखा कुमार है, वह मुस्करा उठा, ‘‘तुम हो ?’’
कुमार भी मुस्कराया, ‘‘तुम क्या समझे थे ?’’
‘‘पुलिस।’’
दोनों हँस पड़े। कुमार बोला, ‘‘इस समय कहाँ जा रहे हो ?’’
‘‘मोहनकृष्ण के घर, तुम भी चलो। बेचारे परदेसी हैं। दो जनों को देखकर ढाढस बँधेगा। ’’
कुमार ने तुरन्त कहा, ‘‘चलो कान्त ! उन लोगों के साथ निस्सन्देह बहुत बुरा हुआ है। घर पर बेचारा अकेला था। माँ और पत्नी बाहर गई हुई थीं। लौटकर उन्होंने उसकी लाश देखी।’’
कान्त का कण्ठ रुँध आया, बोला, ‘‘ओफ़ ! क्या हुआ होगा तब ? ’’
‘‘वही, जो कुछ होता। उन्होंने मरना चाहा, पर मर नहीं सकीं। घण्टों तक वे लाश के पास बैठी रहीं। बहुत देर बाद हमने जाकर देखा कि उसकी पत्नी संज्ञाहीन पड़ी है और माँ पागल-सी शून्य में ताक रही है। हमें देखकर माँ ने जो करुण गुहार की उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा कि अभी जाकर संसार के समस्त मुसलमानों का उसी प्रकार नाश कर डालूँ जिस प्रकार चाणक्य ने नन्द-वंश का किया था। माँ के सामने पुत्र और पत्नी के सामने पतियों की पत्थर मार-मार कर हत्या करूँ और फिर पूछूँ, अब बताओ कैसा लगता है ?’’
कान्त ने एक बार कुमार की ओर देखा और फिर उच्छ्वसित स्वर में बोला, ‘‘ऐसे समय बड़े-बड़ों का धीरज छूट जाता है कुमार !’’
‘‘जानता हूँ कान्त !’’ कुमार ने कहा, ‘‘पर सोचो तो जब मेरा यह हाल हुआ तो साधरण जनता क्या-क्या न सोचती होगी ?’’
कान्त हँस पड़ा, ‘‘वह जो-कुछ सोच सकती है उसी का परिणाम तो भुगत रहे हैं। परन्तु......’’
वह अपना वाक्य पूरा कर भी न पाया था कि उसने पाया वे हेडमास्टर साहब के घर के सामने खड़े हैं।
अन्दर जाकर उन्होंने देखा कि सामने के ओसारे में कई छाया-मूर्तियाँ चित्रलिपि की तरह निस्तब्ध-मौन और संज्ञाहीन पड़ी हैं लेकिन उन्हें पहचानते ही वहाँ एक गहरा चीत्कार उठा, ‘‘मास्टरजी ! मेरा बच्चा मेरा लाल कहाँ गया ?’’
कांत यहीं कच्चा है। वह स्वयं रो पड़ा; पर ठीक समय पर कुमार ने उसकी सहायता की। संवेदना के स्वर में वह बोला, ‘‘माताजी ! आपका पुत्र शहीद हुआ है। शहीदों के लिए रोया नहीं करते।’’
परन्तु रुदन नहीं रुका। यद्यपि गला बैठ गया था, तो भी पीड़ा का ज्वर जैसे उसमें से उमड़ा पड़ता था। वह दीवार से सिर टिकाये रो रही थीं, दो स्त्रियों ने उन्हें थामा हुआ था। और कमला....एक कोने में वह बैठी थी। कान्त ने देखा-उसने दोनों हाथों से मुँह ढक रखा है। उसकी सांस बड़ी तेजी से उठती है पर बाहर निकलने का रास्ता नहीं है; इसलिए वह तड़प रही है। उसने सोचा-क्या कहूँ इससे ? इसे सांत्वना देनी चाहिए, परन्तु ढूँढ़ने पर भी शब्द नहीं मिल रहे हैं। उसे अपने ऊपर ग्लानि हो आई परन्तु कभी कुमार फिर स्नेह-सिंचित स्वर में बोला, ‘‘माँजी ! आपको सब्र करना ही होगा। आप न करेंगी तो बहू किसका मुँह देखेगी....’’
बहू का नाम सुनकर चीत्कार और भी गहरा हो उठा, ‘‘हाय ! वह मर क्यों न गई ? क्यों नहीं उन पापियों ने उसे मार डाला ? हाय, मैं क्यों चली गई थी ? हाय.....’’
एकाएक अब कान्त का स्वर फूटा। वह बोला, ‘‘आप होतीं भी तो क्या कर लेंती ?’’
‘‘करती क्या मास्टरजी ! मैं उनसे कहती-मुझे मार डालो, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। हाय, मैं अब क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? यह क्या हुआ ? एक क्षण में मेरा स्वर्ग नरक कैसे बन गया मास्टरजी ? मैंने भगवान् का क्या बिगाड़ा था.....?’’
फिर वही भगवान् की बात-इस स्थिति में भी कान्त का मन विद्रोह से भर उठा, मनुष्य इतना कायर क्यों है ? वह रोता क्यों है ? मोहन एक व्यक्ति था। उसका दर्द व्यक्ति का दर्द था। उसे संसार पर लादने की व्यर्थ चेष्टा क्यों ? वह चला गया। उसके बिना रुका क्या है ? संसार उसी गति से चल रहा है। धरती घूम रही है तारे मुस्करा रहे हैं।
भगवान का नाम सुनकर रामनाथ का दर्द और भी टीस उठा, ‘‘भगवान का मैंने क्या बिगाड़ा था ? उसने मेरे बेटे को मुझेसे क्यों छीना ?’’
उसी समय उसने निशिकान्त और पण्डितजी को देखा। वे दोनों चुपचाप एक कोने में जा बैठे थे। उन्हें देखकर रामनाथ और भी ज़ोर से रो उठा, ‘‘पण्डितजी, पण्डितजी ! मैं क्या करूँ ?’’
पण्डितजी ने दृढ़ स्वर में कहा, ‘‘तुम्हारा बेटा बहादुर था वह शहीद की मौत मरा है, उसके लिए रोते हो ?’’
निशिकान्त सान्त्वना के स्वर में बोला, ‘‘रामनाथ जी ! तुम्हारा दुःख बहुत बड़ा है, पर अब क्या हो सकता है ? तुम रोओगे तो तुम्हारे बच्चों को कौन सँभालेगा ? उनकी माँ भी तो नहीं है।’’
‘‘ठीक है कान्त भइया ! पर....पर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था ? ’’
पण्डितजी तड़प उठे, ‘‘भगवान् मेरा जाने, तुम्हें यही पता नहीं कि जो बिगाड़ने वाले होते हैं वे कभी सामने नहीं आते। वे कायर होते हैं।’’
वहाँ बैठे हुए आदमियों में से एक ने इस बात का समर्थन किया, ‘‘जी हाँ ! आप ठीक कहते हैं, उन्होंने घर के अन्दर से गोली चलाई।’’ दूसरे ने कहा, ‘‘यही तो। वे अन्दर थे और हिन्दू बाहर।’’
‘‘हिन्दू कायर हैं, नहीं तो.....’’
‘‘नहीं तो क्या ?’’ निशिकान्त एकाएक पूछ बैठा।
जिनसे पूछा गया था वह एक बार तो सकपका गये, पर फिर दृढ़ स्वर में बोले, ‘‘बाबूजी ! आपको क्या पता ? मैं जानता हूँ, हिन्दुओं ने रायबहादुर से कहा था, ‘‘एक बार अपनी बन्दूक दे दो, फिर हम देख लेंगे’, लेकिन रायबहादुर ! वह हिन्दू थे और हिन्दू होते हैं दयालु, अहिंसा के पुजारी। सो उसका फल उन्होंने भोगा। आप मरे और साथ में चार को और ले गये ।’’
‘‘हाँ, बेचारे चारों ही निर्दोष मारे गये। रामनाथ का लड़का स्कूल से लौट रहा था.....’’
‘‘चिम्मा कुम्हार के बेटे ने समझा था कि कोई तमाशा हो रहा है।’’
‘‘और लाला देवादीन तो खाना खाने घर जा रहे थे।’’
‘‘और बाबू मोहनकृष्ण ! वह बेचारा तो अपने घर में बैठा था।’’
‘‘बाबू मोहनकृष्ण,’’ निशिकान्त ने धीरे से कहा, ‘‘जो उन्हें जानते हैं वे किसी भी शर्त पर यह नहीं मान सकेंगे कि मोहनकृष्ण मुसलमानों से लड़ सकता है।’’
‘‘और उसी आदमी को मुसलमानों ने मार डाला।’’ रामनाथ ने आह भरकर कहा, ‘‘न जाने भगवान् क्या चाहते हैं ! मुझे ही देखो, मैंने जन्म-भर कांग्रेस की सेवा की है और मेरा बच्चा मुसलमानों के हाथों मारा गया। दुनिया क्या कहेगी ?’’
‘‘कहेगी क्या ?’’ पण्डितजी ने कहा, ‘‘और कहेगी भी तो तुम फिक्र क्यों करते हो। जो होना था, हो चुका। तुम मर नहीं सकते। और मरो भी क्यों ? जीओ और शान से जीओ।’’
और फिर उठते-उठते कहा, ‘‘रामनाथ, मैं कहता हूँ कि रोज सवेरे रामायण का पाठ किया करो। भगवान् मेरा जाने, रामायण से बढ़कर कोई पुस्तक इस संसार में नहीं है। राजनीति, धर्म और आचरण, सभी कुछ उसमें है। पढ़कर मन को शान्ति मिलती है और तुम्हारा जी न लगे तो मेरे पास आ जाया करो।’’
और वे विदा माँगकर बाहर आ गये। सड़क की बिजली जल चुकी थी और उसका गदराया हुआ प्रकाश अन्धकार के साथ गलबाहीं डाले इधर-उधर बिखरा पड़ा था। सन्नाटा ऐसा था कि कभी-कभी उन लोगों के अपने के अपने ही पदचाप उनके भय का कारण बन जाते थे। वे कुछ दूर तक चुपचाप बिना बोले चलते रहे।
फिर सहसा पण्डितजी बोल उठे, ‘‘देखा निशिकान्त ! यह हमारी सहानुभूति है। कितने आदमी थे इसके पास !’’
निशिकान्त ने कहा, ‘‘आदमी देखना चाहते हो तो रायबहादुर के घर चलो ।’’
रायबहादुर का नाम सुनते ही पण्डितजी को क्रोध आ गया। बोले, ‘‘मैं वहाँ नहीं जाऊँगा।’’
‘‘सोचता मैं भी यही हूँ।’’
पण्डितजी ने कहा, ‘‘हम कितने बेईमान हैं। रामनाथ कांग्रेस का कितना काम करता है ! नेता सजे-सजाये रंगमंच पर लैक्चर देकर चले जाते हैं, परन्तु सभा का प्रबन्ध करना और उसका संदेश घर-घर पहुँचाना इसी का काम है। यह इस भवन की नींव है, परन्तु इसीलिए आज इसके पास कोई नहीं है।’’
निशिकान्त उनकी ओर देखकर बोला, ‘‘पण्डितजी ! नींव आँखों से ओझल रहती है। उसके पास कोई नहीं जा सकता, लेकिन यही उसकी शक्ति है। सहानुभूति के अभाव में ही आदमी अपने पैरों खड़ा होना सीखता है।’’
पण्डितजी ने तलखी से जवाब दिया, ‘‘निशिकान्त ! यह सब बेईमानी है। मैं पूछता हूँ, आखिर क्यों सब लोग रायबहादुर के घर गये और रामनाथ के पास नहीं आये ?’’
निशिकान्त के मुँह से दीर्घ निश्वास निकल गया। ऊपर देखता हुआ वह धीरे से बोला, ‘‘पण्डितजी ! इस प्रश्न का उत्तर है। उत्तर सभी प्रश्नों का होता है, परन्तु केवल उत्तर से प्रश्न हल नहीं होता। हल उत्तर के विश्लेषण और फिर विश्लेषण के निष्कर्षों पर अमल करने से होता है।’’
‘‘तो ठीक है, मैं रायबहादुर के घर नहीं जाऊँगा। चिम्मा कुम्हार के घर चलो। ’’
‘‘चलिये ! लेकिन देर हो चली है। आठ बजे तक हमें घर पहुँच जाना चाहिए।’’
यह कहकर उसने फिर ऊपर देखा। सप्तर्षि-मण्डल मकानों के पीछे से उठकर ऊपर आ गया था और व्याध हरिणियों पर तीर साधे मंत्र की भांति आगे बढ़ रहा था। उसके मन में उठा, कितने शान्त और कितने सुन्दर हैं ये तारागण ! क्या इन्होंने कल होने वाले रक्त-पात को नहीं देखा ? क्या ये नहीं जानते कि रायबहादुर ने बन्दूक नहीं चलाई थी ?
पण्डितजी बोल उठे, ‘‘भाई, अब सबके घर नहीं जा सकते।’’
‘‘मैं भी यही सोचता हूँ।’’
‘‘एक स्थान पर और हो आते हैं। बाकी कल चलेंगे।’’
निशिकान्त ने क्षण-भर सोचकर कहा, ‘‘पण्डितजी, आज और कल में बड़ा अन्तर है।’’
‘‘तो ?’’
‘‘ऐसा करिये। आप चिम्पा के घर चले जाइये। मैं मोहनकृष्ण के घर जा रहा हूँ, वहाँ तो मुझे कल ही जाना चाहिए था।’’
‘‘मैं जानता हूँ, तुमने उसकी स्त्री को पढ़ाया है।’’
और फिर वे दोनों दो रास्तों पर मुड़ गये। तब तक चाँद निकल आया था और उसका धीमा पर शान्त प्रकाश धरती के विषाद को दूर करने के लिए धीरे-धीरे नीचे उतर रहा था। निशिकान्त का मन फिर अवसाद से भरने लगा। उससे बचने के लिए उसने तेजी से चलना शुरू किया; परन्तु दूसरे क्षण ही वह भयंकर वेग से काँप उठा। किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। देखा कुमार है, वह मुस्करा उठा, ‘‘तुम हो ?’’
कुमार भी मुस्कराया, ‘‘तुम क्या समझे थे ?’’
‘‘पुलिस।’’
दोनों हँस पड़े। कुमार बोला, ‘‘इस समय कहाँ जा रहे हो ?’’
‘‘मोहनकृष्ण के घर, तुम भी चलो। बेचारे परदेसी हैं। दो जनों को देखकर ढाढस बँधेगा। ’’
कुमार ने तुरन्त कहा, ‘‘चलो कान्त ! उन लोगों के साथ निस्सन्देह बहुत बुरा हुआ है। घर पर बेचारा अकेला था। माँ और पत्नी बाहर गई हुई थीं। लौटकर उन्होंने उसकी लाश देखी।’’
कान्त का कण्ठ रुँध आया, बोला, ‘‘ओफ़ ! क्या हुआ होगा तब ? ’’
‘‘वही, जो कुछ होता। उन्होंने मरना चाहा, पर मर नहीं सकीं। घण्टों तक वे लाश के पास बैठी रहीं। बहुत देर बाद हमने जाकर देखा कि उसकी पत्नी संज्ञाहीन पड़ी है और माँ पागल-सी शून्य में ताक रही है। हमें देखकर माँ ने जो करुण गुहार की उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा कि अभी जाकर संसार के समस्त मुसलमानों का उसी प्रकार नाश कर डालूँ जिस प्रकार चाणक्य ने नन्द-वंश का किया था। माँ के सामने पुत्र और पत्नी के सामने पतियों की पत्थर मार-मार कर हत्या करूँ और फिर पूछूँ, अब बताओ कैसा लगता है ?’’
कान्त ने एक बार कुमार की ओर देखा और फिर उच्छ्वसित स्वर में बोला, ‘‘ऐसे समय बड़े-बड़ों का धीरज छूट जाता है कुमार !’’
‘‘जानता हूँ कान्त !’’ कुमार ने कहा, ‘‘पर सोचो तो जब मेरा यह हाल हुआ तो साधरण जनता क्या-क्या न सोचती होगी ?’’
कान्त हँस पड़ा, ‘‘वह जो-कुछ सोच सकती है उसी का परिणाम तो भुगत रहे हैं। परन्तु......’’
वह अपना वाक्य पूरा कर भी न पाया था कि उसने पाया वे हेडमास्टर साहब के घर के सामने खड़े हैं।
अन्दर जाकर उन्होंने देखा कि सामने के ओसारे में कई छाया-मूर्तियाँ चित्रलिपि की तरह निस्तब्ध-मौन और संज्ञाहीन पड़ी हैं लेकिन उन्हें पहचानते ही वहाँ एक गहरा चीत्कार उठा, ‘‘मास्टरजी ! मेरा बच्चा मेरा लाल कहाँ गया ?’’
कांत यहीं कच्चा है। वह स्वयं रो पड़ा; पर ठीक समय पर कुमार ने उसकी सहायता की। संवेदना के स्वर में वह बोला, ‘‘माताजी ! आपका पुत्र शहीद हुआ है। शहीदों के लिए रोया नहीं करते।’’
परन्तु रुदन नहीं रुका। यद्यपि गला बैठ गया था, तो भी पीड़ा का ज्वर जैसे उसमें से उमड़ा पड़ता था। वह दीवार से सिर टिकाये रो रही थीं, दो स्त्रियों ने उन्हें थामा हुआ था। और कमला....एक कोने में वह बैठी थी। कान्त ने देखा-उसने दोनों हाथों से मुँह ढक रखा है। उसकी सांस बड़ी तेजी से उठती है पर बाहर निकलने का रास्ता नहीं है; इसलिए वह तड़प रही है। उसने सोचा-क्या कहूँ इससे ? इसे सांत्वना देनी चाहिए, परन्तु ढूँढ़ने पर भी शब्द नहीं मिल रहे हैं। उसे अपने ऊपर ग्लानि हो आई परन्तु कभी कुमार फिर स्नेह-सिंचित स्वर में बोला, ‘‘माँजी ! आपको सब्र करना ही होगा। आप न करेंगी तो बहू किसका मुँह देखेगी....’’
बहू का नाम सुनकर चीत्कार और भी गहरा हो उठा, ‘‘हाय ! वह मर क्यों न गई ? क्यों नहीं उन पापियों ने उसे मार डाला ? हाय, मैं क्यों चली गई थी ? हाय.....’’
एकाएक अब कान्त का स्वर फूटा। वह बोला, ‘‘आप होतीं भी तो क्या कर लेंती ?’’
‘‘करती क्या मास्टरजी ! मैं उनसे कहती-मुझे मार डालो, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। हाय, मैं अब क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? यह क्या हुआ ? एक क्षण में मेरा स्वर्ग नरक कैसे बन गया मास्टरजी ? मैंने भगवान् का क्या बिगाड़ा था.....?’’
फिर वही भगवान् की बात-इस स्थिति में भी कान्त का मन विद्रोह से भर उठा, मनुष्य इतना कायर क्यों है ? वह रोता क्यों है ? मोहन एक व्यक्ति था। उसका दर्द व्यक्ति का दर्द था। उसे संसार पर लादने की व्यर्थ चेष्टा क्यों ? वह चला गया। उसके बिना रुका क्या है ? संसार उसी गति से चल रहा है। धरती घूम रही है तारे मुस्करा रहे हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book