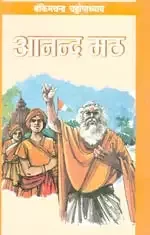|
सदाबहार >> आनन्द मठ आनन्द मठबंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय
|
393 पाठक हैं |
||||||
बंकिमचन्द्र का उत्कृष्ट लेखन सामाजिक और तात्कालिक पृष्ठभूमि में।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय बंगला के शीर्षस्थ उपन्यासकार हैं। उनकी लेखनी से
बंगाल साहित्य तो समृद्ध हुआ ही है, हिन्दी भी उपकृत हुई है। उनकी
लोकप्रियता का यह आलम है कि पिछले डेढ़ सौ सालों से उनके उपन्यास विभिन्न
भाषाओं में अनूदित हो रहे हैं और कई-कई संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। उनके
उपन्यासों में नारी की अन्तर्वेदना व उसकी शक्तिमत्ता बेहद प्रभावशाली ढंग
से अभिव्यक्त हुई है। उनके उपन्यासों में नारी की गरिमा को नयी पहचान मिली
है और भारतीय इतिहास को समझने की नयी दृष्टि।
वे ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे। वे भारत के एलेक्जेंडर
ड्यूमा माने जाते हैं।
‘‘हरे मुरारे मधुकैटभारे।
ब्रह्मचारी ने इस पर दीर्घ-निश्वास छोड़कर
कहा, ‘‘माँ
इस घोर व्रत में बलिदान है हम सबको अपनी बलि देनी पड़ेगी। मैं मरूंगा,
जीवानंद, भवानंद, सभी मरेंगे, लगता है माँ तुम भी मरोगी। किन्तु देखो, काम
करके मरना होगा, बिना काम किये मरना क्या अच्छा है ? मैंन केवल देश को माँ
कहा है, इसके अलावा और किसी को माँ नहीं कहा। क्योंकि उसी सुजला, सुफला
धरनी के अलावा अन्य मातृक है। और तुम्हें माँ कहा है, तुम माँ होकर सन्तान
का काम करती हो। जिससे कार्योद्धार हो, वही करना, जीवानंद के प्राणों की
रक्षा करना।’’
यह कह कर सत्यानंद ‘हरे मुरारे मधुकैटभारे’ गाते-गाते
वहां से चले गए।
(इसी पुस्तक से)
उपक्रमणिका
दूर-दूर तक फैला हुआ जंगल जंगल में ज्यादातर
पेड़ शाल के थे, लेकिन इनके
अलावा और भी कई तरह के पेड़ थे। शाखाओं और पत्तों से जुड़े हुए पेड़ों की
अनंत श्रेणी दूर तक चली गयी थी। विच्छेद-शून्य, छिद्र-शून्य रोशनी के आने
के जरा से मार्ग से भी विहीन ऐसे घनीभूत पत्तों का अनंत समुद्र कोस दर
कोस, कोस दर कोस पवन की तरंगों पर तरंग छोड़ता हुआ सर्वत्र व्याप्त था।
नीचे अंधकार। दोपहर में भी रोशनी का अभाव था। भयानक वातावरण। इस जगंल के
अन्दर से कभी कोई आदमी नहीं गुजरता। पत्तों की निरन्तर मरमर तथा जंगली
पशुपक्षियों के स्वर के अलावा कोई और आवाज इस जगंल के अंदर नहीं सुनाई
देती।
एक तो यह विस्तृत अत्यंत निबिड़ अंधकारमय जंगल, उस पर रात का समय। रात का दूसरा पहर था। रात बेहद काली थी। जंगल के बाहर भी अंधकार था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। जंगल के भीतर का अंधकार पाताल जैसे अंधकार की तरह था।
पशु-पक्षी बिल्कुल निस्तब्ध थे। जंगल में लाखों-करोड़ों पशु-पक्षी, कीट-पतंग रहते थे। कोई भी आवाज नहीं कर रहा था। बल्कि उस अंधकार को अनुभव किया जा सकता था, शब्दमयी पृथ्वी का वह निशब्द भाव अनुभव नहीं किया जा सकता।
उस असीम जंगल में, उस सूचीभेद्य अंधकारमय रात में, उस अनुभवहीन निस्तब्धता में एकाएक आवाज हुई, ‘‘मेरी मनोकामना क्या सिद्ध नहीं होगी ?’’
आवाज गूँजकर फिर उस जंगल की निस्तब्धता में डूब गई। कौन कहेगा कि उस जंगल में किसी आदमी की आवाज सुनाई दी थी ? कुछ देर के बाद फिर आवाज हुई, फिर उस निस्तब्धता को चीरती आदमी की आवाज सुनाई दी, ‘‘मेरी मनेकामना क्या सिद्ध नहीं होगी ?’’
इस प्रकार तीन बार वह अंधकार समुद्र आलोड़ित हुआ, तब जवाब मिला, ‘‘तुम्हारा प्रण क्या है’’
‘‘मेरी जीवन-सर्वस्व।’’
‘‘जीवन तो तुच्छ है, सभी त्याग सकते हैं।’’
‘‘और क्या है ? और क्या दूँ ?’’
जवाब मिला, ‘‘भक्ति।’’
एक तो यह विस्तृत अत्यंत निबिड़ अंधकारमय जंगल, उस पर रात का समय। रात का दूसरा पहर था। रात बेहद काली थी। जंगल के बाहर भी अंधकार था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। जंगल के भीतर का अंधकार पाताल जैसे अंधकार की तरह था।
पशु-पक्षी बिल्कुल निस्तब्ध थे। जंगल में लाखों-करोड़ों पशु-पक्षी, कीट-पतंग रहते थे। कोई भी आवाज नहीं कर रहा था। बल्कि उस अंधकार को अनुभव किया जा सकता था, शब्दमयी पृथ्वी का वह निशब्द भाव अनुभव नहीं किया जा सकता।
उस असीम जंगल में, उस सूचीभेद्य अंधकारमय रात में, उस अनुभवहीन निस्तब्धता में एकाएक आवाज हुई, ‘‘मेरी मनोकामना क्या सिद्ध नहीं होगी ?’’
आवाज गूँजकर फिर उस जंगल की निस्तब्धता में डूब गई। कौन कहेगा कि उस जंगल में किसी आदमी की आवाज सुनाई दी थी ? कुछ देर के बाद फिर आवाज हुई, फिर उस निस्तब्धता को चीरती आदमी की आवाज सुनाई दी, ‘‘मेरी मनेकामना क्या सिद्ध नहीं होगी ?’’
इस प्रकार तीन बार वह अंधकार समुद्र आलोड़ित हुआ, तब जवाब मिला, ‘‘तुम्हारा प्रण क्या है’’
‘‘मेरी जीवन-सर्वस्व।’’
‘‘जीवन तो तुच्छ है, सभी त्याग सकते हैं।’’
‘‘और क्या है ? और क्या दूँ ?’’
जवाब मिला, ‘‘भक्ति।’’
प्रथम खण्ड
प्रथम परिच्छेद
बंगला सन् 1176 का ग्रीष्म-काल था।
ऐसे समय एक पदचिन्ह नामक गांव में भयावह गरमी पड़ रही थी। गांव में काफी
तादात में घर थे, मगर कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। बाजार में
कतार-दर-कतार दुकानें थीं, दुकानों में ढेर सारा सामान था, गांव-गांव में
मिट्टी के सैकड़ों घर थे, बीच-बीच में ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएं। मगर आज
चारों तरफ खामोशी थी। बाजारों में दुकानें बंद थीं, दुकानदार कहां भाग गए
थे, इसका कोई ठिकाना नहीं था। आज हाट लगने का दिन था, मगर हाट में एक भी
दुकान नहीं लगी थी। जुलाहे अपने करघे बंद करके घर के एक कोने में पड़े रो
रहे थे। व्यवसायी अपना व्यवसाय भूलकर बच्चों को गोद में लिए रो रहे थे।
दाताओं ने दान बंद कर दिया था, शिक्षकों ने पाठशालाएं बंद कर दी थीं। शिशु
भी सहमे-सहमे से रो रहे थे। राजपथ पर कोई नजर नहीं आ रहा था। सरोवरों में
कोई नहाने वाला भी नहीं था। घरों में लोगों का नामों-निशान नहीं था।
पशु-पक्षी भी नज़र नहीं आ रहे थे। चरने वाली गौएं भी कहीं नज़र नहीं आ रही
थीं। केवल शमशान में सियारों व कुत्तों की आवाजें गूंज रहीं थीं।
सामने एक वृहद अट्टालिका थी। उसके ऊंचे-ऊचे गुबंद दूर से ही नजर आते थे। छोटे-छोटे घरों के जंगल में यह अट्टालिका शैल-शिखर की तरह शोभा पा रही थी। मगर ऐसी शोभा का क्या-अट्टालिका के दरवाजे बंद थे, घर में लोगों का जमावड़ा नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं, अंदर हवा तक प्रवेश नहीं कर पा रही थी। अट्टालिका के अंदर कमरों में दोपहर के बावजूद अंधकार था। उस अंधकार में मुरझाए फूलों-सा एक दम्पत्ति बैठा सोच रहा था। उनके आगे अकाल का रौरव फैला हुआ था।
सन् 1174 में फसल अच्छी हुई नहीं, सो 1175 के साल में हालात बिगड़ गए-लोगों को परेशानी हुई, इसके बावजूद शासकों ने एक-एक कौड़ी तक कर वसूल किया। इस कड़ाई का नतीजा यह हुआ कि गरीबों के घर में एक वक्त चूल्हा जला। सन् 1175 में वर्षा-ऋतु में अच्छी बारिश हुई। लोगों ने सोचा, शायद देवता सदय हुए हैं। सो खुश होकर राखाल ने मैदान में गाना गाया, कृषक पत्नी फिर चांदी की पाजेब के लिए पति से इसरार करने लगी। अकस्मात अश्विन महीने देवता फिर विमुख हो गए। आश्विन और कार्तिक महीने में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। खेतों में धान सूखकर एकदम खड़ी हो गयी। जिनके थोड़े बहुत धान हुआ, उसे राजकर्मियों ने अपने सिपाहियों के लिए खरीद कर रख लिया लोगों को खाने को नहीं मिला। पहले एक शाम उपवास किया, फिर एक बेला अधपेट खाने लगे, इसके बाद दो शामों का उपवास शुरू किया। चैत्र में जो थोड़ी फसल हुई, उससे किसी के मुख में पूरा ग्रास भी नहीं पहुंचा। मगर कर वसूल करने वाला कर्ताधर्ता मोहम्मद रजा खां कुछ और सोचता था। उसका विचार था, यही मौका है कुछ कर दिखाने का। उसने एकदम से दस प्रतिशत कर सब पर ठोंक दिया। सारे बंगाल में रोने-चीखने का कोलाहल मच गया।
लोगों ने पहले भीख माँगना शुरू किया, पर भीख उन्हें कब तक मिलती। उपवास करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इससे यह हुआ कि वे रोगाक्रांत होने लगे। फिर लोगों ने गौएं बेचीं, बैल-हल, बेचे धान का बीज तक खा लिया, घर द्वार बेच दिया, खेती-बाड़ी बेची। इसके बाद कुछ न बचा तो लड़कियां बेचना शुरू कर दिया, फिर लड़के फिर पत्नियां। अब लड़कियां, लड़के और पत्नियां खरीदने वाला भी कोई न बचा। खरीददार रहे नहीं, सभी बेचने वाले थे। खाने की चीजों का अभाव ऐसा दारुण था कि लोग पेड़ के पत्ते खाने लगे, घास खाने लगे, टहनियां और डालियां खाने लगे। जंगली व छोटे लोग कुत्ते, बिल्ली और चूहे खाने लगे। कई लोग भाग गए, जो भागे, वे भी विदेश में जाकर भूखों मर गए। जो नहीं भागे, वे अखाद्य खाकर या अनाहार रहकर रोग में पड़कर मारे गए।
रोग को भी मौका मिल गया-जहां देखो, वहीं बुखार, हैजा, क्षय और चेचक ! इनमें भी चेचक का प्रकोप ज्यादा ही फैल गया था। घर-घर में लोग चेचक से मर रहे थे। कौन किसे जल दे या कौन किसे छुए ! न कोई किसी की दवा-दारु कर पाता, न कोई किसी की देखभाल कर पाता और मरने पर न कोई किसी का शव उठा पाता। अच्छे-अच्छे मकान भी बदबू से ओतप्रोत हो गए थे। जिस घर में एक बार चेचक प्रवेश कर जाता, उस घर के लोग रोगी को अपने हाल पर छोड़ कर भाग निकलते।
महेन्द्र सिंह पदचिन्ह गांव के बहुत बड़े धनवान थे-मगर आज धनी और निर्धन में कोई अंतर नहीं रहा। ऐसी दुखद स्थिति में व्याधिग्रस्त होकर उनके समस्त आत्मीय स्वजन दास-दासी आदि बारी-बारी से चले गए थे। कोई मर गया था तो कोई भाग गया था। उस भरे-पूरे परिवार में अब बचे रहे थे वे स्वयं, उनकी पत्नी और एक शिशु कन्या। उन्हीं की सुना रहा हूं।
उनकी पत्नी कल्याणी चिन्ता त्याग कर गोशाला गयी और खुद ही गाय दुहने लगी। फिर दूध गरम करके बच्ची को पिलाया, इसके बाद गाय को पानी-सानी देने गयी। वापस लौटकर आयी तो महेन्द्र ने पूछा, ‘‘इस तरह कितने दिन चलेगा ?’’
कल्याणी बोली ‘‘ज्यादा दिन तो नहीं। जितने दिन चल सका, जितने दिन मैं चला सकी, चलाऊंगी, इसके बाद तुम बच्ची को लेकर शहर चले जाना।’’
‘‘अगर शहर जाना ही है तो तुम्हें इतना दुःख क्यों सहने दूं। चलो न, इसी समय चलते हैं।’’
दोनों में इस विषय पर खूब तर्क वितर्क होने लगा।
कल्याणी ने पूछा, ‘‘शहर जाकर क्या कोई विशेष उपकार होगा ?’’
महेन्द्र ने जवाब दिया, ‘‘शहर भी शायद ऐसा ही जन-शून्य और प्राण-रक्षा से उपाय शून्य हो।’’
‘‘मुर्शिदाबाद, कासिमबाजार या कलकत्ता जाकर शायद, हमारे प्राण बच जाएं। इस जगह को छोड़कर जाना तो बिल्कुल उचित है।’’
महेन्द्र बोला, ‘‘यह घर एक अरसे से पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचित धन से परिपूर्ण है, हम चले गए तो यह सब चोर लूटकर ले जाएंगे।’’
‘‘अगर लूटने आ गए तो हम दो जने क्या चोरों से धन को बचा पाएंगे। प्राण ही नहीं बचे तो धन का उपभोग कौन करेगा ? चलो, इसी समय सब कुछ बांध-बूंध कर यहां से निकल चलें। अगर प्राण बच गए तो वापस आकर इनका उपभोग करेंगे।’’
महेन्द्र ने पूछा, ‘‘तुम क्या पैदल चल सकोगी ? पालकी ढोने वाले तो सब मर गए, बैल हैं तो गाड़ीवान नहीं, गाड़ीवान हैं तो बैल नहीं।’’
‘‘मैं पैदल चल सकती हूं, तुम चिन्ता मत करना।’’
कल्याणी ने मन ही मन तय कर लिया था भले ही मैं रास्ते में मारी जाऊं, फिर भी ये दोनो तो बचे रहेंगे।
अगले दिन सुबह दोनों ने कुछ रुपये पैसे गांठ में बांध लिए, घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया, गाय-बैल खुले छोड़ दिए और बच्ची को गोद में उठाकर राजधानी की ओर सफर शुरू कर दिया। सफर के दौरान महेन्द्र बोले, ‘‘रास्ता बेहद दुर्गम है। कदम-कदम पर लुटेरे घूम रहे हैं, खाली हाथ निकलना उचित नहीं।’’ यह कहकर महेन्द्र घर में वापस गया और बंदूक-गोली बारूद उठा लाया।
यह देखकर कल्याणी बोली, ‘‘अगर अस्त्र की बात याद आयी है तो तुम जरा सुकुमारी को पकड़ो, मैं भी हथियार लेकर आती हूं।’’ यह कहकर कल्याणी ने बच्ची महेन्द्र की गोद में डाल दी और घर में घुस गयी।
महेन्द्र ने पूछा, ‘‘तुम भला कौन-सा हथियार लेकर चलोगी ?’’
कल्याणी ने घर में आकर जहर की एक छोटी-सी शीशी उठायी और कपड़े में अच्छी तरह छिपा ली। इन दुःख के दिनों में किस्मत में न जाने कब क्या बदा हो-यही सोचकर कल्याणी ने पहले ही जहर का इन्तजाम कर रखा था।
जेठ का महीना था। तेज धूप पड़ रही थी। धरती आग से जल रही थी। हवा में आग मचल रही थी। आकाश गरम तवे की तरह झुलस रहा था। रास्ते की धूल में आग के शोले दहक रहे थे। कल्याणी पसीने से तर-बतर हो गयी। कभी बबूल के पेड़ की छाया में बैठ जाती तो कभी खजूर के पेड़ की। प्यास लगती तो सूखे तालाब का कीचड़ सना पानी पी लेती। इस तरह बेहद तकलीफ से वह रास्ता तय कर रही थी। बच्ची महेन्द्र की गोद में थी-बीच-बीच में महेन्द्र बच्ची को हवा करते जाते थे।
चलते-चलते थक गए तो दोनों हरे-हरे पत्तों से भरे संगठित फूलों से युक्त लता वेष्टित पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। महेन्द्र कल्याणी की सहनशीलता देखकर आश्चर्यचकित थे। पास ही एक सरोवर से वस्त्र भिगोकर महेन्द्र ने अपना और कल्याणी का मुंह, हाथ और सिर सिंचित किया। कल्याणी को थोड़ा चैन मिला, मगर दोनों भूख से बेहद व्याकुल हो गये। यह भी दोनों सहन करने में सक्षम थे, मगर बच्ची की भूख-प्यास सहन करना मुश्किल था। सो वे फिर रास्ते पर चल पड़े। उस अग्निपथ को पार करते हुए वे दोनों शाम से पहले एक बस्ती में पहुंचे महेन्द्र को मन ही मन आशा थी कि बस्ती में पहुंचकर पत्नी व बच्ची के मुंह में शीतल जल दे सकेंगे, प्राण-रक्षा के लिए दो कौर भी नसीब होंगे। लेकिन कहां ? बस्ती में तो एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। बड़े-बड़े घरों में सन्नाटा छाया हुआ था, सारे लोग वहां से भाग चुके थे। महेन्द्र ने इधर-उधर देखने के बाद बच्ची को एक मकान में ले जाकर लिटा दिया। बाहर आकर वे ऊंचे स्वर में बुलाने पुकारने लगे। मगर उन्हें कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला।
वे कल्याणी से बोले, ‘‘सुनो, तुम जरा हिम्मत बांधकर यहां अकेली बैठो यहां अगर गाय हुई तो श्रीकृष्ण की दया से मैं दूध ला रहा हूं।’’
यह कहकर उन्होंने मिट्टी की एक कलसी उठाई और घर से बाहर निकले। वहां कई कलसियां पड़ी थीं।
सामने एक वृहद अट्टालिका थी। उसके ऊंचे-ऊचे गुबंद दूर से ही नजर आते थे। छोटे-छोटे घरों के जंगल में यह अट्टालिका शैल-शिखर की तरह शोभा पा रही थी। मगर ऐसी शोभा का क्या-अट्टालिका के दरवाजे बंद थे, घर में लोगों का जमावड़ा नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं, अंदर हवा तक प्रवेश नहीं कर पा रही थी। अट्टालिका के अंदर कमरों में दोपहर के बावजूद अंधकार था। उस अंधकार में मुरझाए फूलों-सा एक दम्पत्ति बैठा सोच रहा था। उनके आगे अकाल का रौरव फैला हुआ था।
सन् 1174 में फसल अच्छी हुई नहीं, सो 1175 के साल में हालात बिगड़ गए-लोगों को परेशानी हुई, इसके बावजूद शासकों ने एक-एक कौड़ी तक कर वसूल किया। इस कड़ाई का नतीजा यह हुआ कि गरीबों के घर में एक वक्त चूल्हा जला। सन् 1175 में वर्षा-ऋतु में अच्छी बारिश हुई। लोगों ने सोचा, शायद देवता सदय हुए हैं। सो खुश होकर राखाल ने मैदान में गाना गाया, कृषक पत्नी फिर चांदी की पाजेब के लिए पति से इसरार करने लगी। अकस्मात अश्विन महीने देवता फिर विमुख हो गए। आश्विन और कार्तिक महीने में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। खेतों में धान सूखकर एकदम खड़ी हो गयी। जिनके थोड़े बहुत धान हुआ, उसे राजकर्मियों ने अपने सिपाहियों के लिए खरीद कर रख लिया लोगों को खाने को नहीं मिला। पहले एक शाम उपवास किया, फिर एक बेला अधपेट खाने लगे, इसके बाद दो शामों का उपवास शुरू किया। चैत्र में जो थोड़ी फसल हुई, उससे किसी के मुख में पूरा ग्रास भी नहीं पहुंचा। मगर कर वसूल करने वाला कर्ताधर्ता मोहम्मद रजा खां कुछ और सोचता था। उसका विचार था, यही मौका है कुछ कर दिखाने का। उसने एकदम से दस प्रतिशत कर सब पर ठोंक दिया। सारे बंगाल में रोने-चीखने का कोलाहल मच गया।
लोगों ने पहले भीख माँगना शुरू किया, पर भीख उन्हें कब तक मिलती। उपवास करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इससे यह हुआ कि वे रोगाक्रांत होने लगे। फिर लोगों ने गौएं बेचीं, बैल-हल, बेचे धान का बीज तक खा लिया, घर द्वार बेच दिया, खेती-बाड़ी बेची। इसके बाद कुछ न बचा तो लड़कियां बेचना शुरू कर दिया, फिर लड़के फिर पत्नियां। अब लड़कियां, लड़के और पत्नियां खरीदने वाला भी कोई न बचा। खरीददार रहे नहीं, सभी बेचने वाले थे। खाने की चीजों का अभाव ऐसा दारुण था कि लोग पेड़ के पत्ते खाने लगे, घास खाने लगे, टहनियां और डालियां खाने लगे। जंगली व छोटे लोग कुत्ते, बिल्ली और चूहे खाने लगे। कई लोग भाग गए, जो भागे, वे भी विदेश में जाकर भूखों मर गए। जो नहीं भागे, वे अखाद्य खाकर या अनाहार रहकर रोग में पड़कर मारे गए।
रोग को भी मौका मिल गया-जहां देखो, वहीं बुखार, हैजा, क्षय और चेचक ! इनमें भी चेचक का प्रकोप ज्यादा ही फैल गया था। घर-घर में लोग चेचक से मर रहे थे। कौन किसे जल दे या कौन किसे छुए ! न कोई किसी की दवा-दारु कर पाता, न कोई किसी की देखभाल कर पाता और मरने पर न कोई किसी का शव उठा पाता। अच्छे-अच्छे मकान भी बदबू से ओतप्रोत हो गए थे। जिस घर में एक बार चेचक प्रवेश कर जाता, उस घर के लोग रोगी को अपने हाल पर छोड़ कर भाग निकलते।
महेन्द्र सिंह पदचिन्ह गांव के बहुत बड़े धनवान थे-मगर आज धनी और निर्धन में कोई अंतर नहीं रहा। ऐसी दुखद स्थिति में व्याधिग्रस्त होकर उनके समस्त आत्मीय स्वजन दास-दासी आदि बारी-बारी से चले गए थे। कोई मर गया था तो कोई भाग गया था। उस भरे-पूरे परिवार में अब बचे रहे थे वे स्वयं, उनकी पत्नी और एक शिशु कन्या। उन्हीं की सुना रहा हूं।
उनकी पत्नी कल्याणी चिन्ता त्याग कर गोशाला गयी और खुद ही गाय दुहने लगी। फिर दूध गरम करके बच्ची को पिलाया, इसके बाद गाय को पानी-सानी देने गयी। वापस लौटकर आयी तो महेन्द्र ने पूछा, ‘‘इस तरह कितने दिन चलेगा ?’’
कल्याणी बोली ‘‘ज्यादा दिन तो नहीं। जितने दिन चल सका, जितने दिन मैं चला सकी, चलाऊंगी, इसके बाद तुम बच्ची को लेकर शहर चले जाना।’’
‘‘अगर शहर जाना ही है तो तुम्हें इतना दुःख क्यों सहने दूं। चलो न, इसी समय चलते हैं।’’
दोनों में इस विषय पर खूब तर्क वितर्क होने लगा।
कल्याणी ने पूछा, ‘‘शहर जाकर क्या कोई विशेष उपकार होगा ?’’
महेन्द्र ने जवाब दिया, ‘‘शहर भी शायद ऐसा ही जन-शून्य और प्राण-रक्षा से उपाय शून्य हो।’’
‘‘मुर्शिदाबाद, कासिमबाजार या कलकत्ता जाकर शायद, हमारे प्राण बच जाएं। इस जगह को छोड़कर जाना तो बिल्कुल उचित है।’’
महेन्द्र बोला, ‘‘यह घर एक अरसे से पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचित धन से परिपूर्ण है, हम चले गए तो यह सब चोर लूटकर ले जाएंगे।’’
‘‘अगर लूटने आ गए तो हम दो जने क्या चोरों से धन को बचा पाएंगे। प्राण ही नहीं बचे तो धन का उपभोग कौन करेगा ? चलो, इसी समय सब कुछ बांध-बूंध कर यहां से निकल चलें। अगर प्राण बच गए तो वापस आकर इनका उपभोग करेंगे।’’
महेन्द्र ने पूछा, ‘‘तुम क्या पैदल चल सकोगी ? पालकी ढोने वाले तो सब मर गए, बैल हैं तो गाड़ीवान नहीं, गाड़ीवान हैं तो बैल नहीं।’’
‘‘मैं पैदल चल सकती हूं, तुम चिन्ता मत करना।’’
कल्याणी ने मन ही मन तय कर लिया था भले ही मैं रास्ते में मारी जाऊं, फिर भी ये दोनो तो बचे रहेंगे।
अगले दिन सुबह दोनों ने कुछ रुपये पैसे गांठ में बांध लिए, घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया, गाय-बैल खुले छोड़ दिए और बच्ची को गोद में उठाकर राजधानी की ओर सफर शुरू कर दिया। सफर के दौरान महेन्द्र बोले, ‘‘रास्ता बेहद दुर्गम है। कदम-कदम पर लुटेरे घूम रहे हैं, खाली हाथ निकलना उचित नहीं।’’ यह कहकर महेन्द्र घर में वापस गया और बंदूक-गोली बारूद उठा लाया।
यह देखकर कल्याणी बोली, ‘‘अगर अस्त्र की बात याद आयी है तो तुम जरा सुकुमारी को पकड़ो, मैं भी हथियार लेकर आती हूं।’’ यह कहकर कल्याणी ने बच्ची महेन्द्र की गोद में डाल दी और घर में घुस गयी।
महेन्द्र ने पूछा, ‘‘तुम भला कौन-सा हथियार लेकर चलोगी ?’’
कल्याणी ने घर में आकर जहर की एक छोटी-सी शीशी उठायी और कपड़े में अच्छी तरह छिपा ली। इन दुःख के दिनों में किस्मत में न जाने कब क्या बदा हो-यही सोचकर कल्याणी ने पहले ही जहर का इन्तजाम कर रखा था।
जेठ का महीना था। तेज धूप पड़ रही थी। धरती आग से जल रही थी। हवा में आग मचल रही थी। आकाश गरम तवे की तरह झुलस रहा था। रास्ते की धूल में आग के शोले दहक रहे थे। कल्याणी पसीने से तर-बतर हो गयी। कभी बबूल के पेड़ की छाया में बैठ जाती तो कभी खजूर के पेड़ की। प्यास लगती तो सूखे तालाब का कीचड़ सना पानी पी लेती। इस तरह बेहद तकलीफ से वह रास्ता तय कर रही थी। बच्ची महेन्द्र की गोद में थी-बीच-बीच में महेन्द्र बच्ची को हवा करते जाते थे।
चलते-चलते थक गए तो दोनों हरे-हरे पत्तों से भरे संगठित फूलों से युक्त लता वेष्टित पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। महेन्द्र कल्याणी की सहनशीलता देखकर आश्चर्यचकित थे। पास ही एक सरोवर से वस्त्र भिगोकर महेन्द्र ने अपना और कल्याणी का मुंह, हाथ और सिर सिंचित किया। कल्याणी को थोड़ा चैन मिला, मगर दोनों भूख से बेहद व्याकुल हो गये। यह भी दोनों सहन करने में सक्षम थे, मगर बच्ची की भूख-प्यास सहन करना मुश्किल था। सो वे फिर रास्ते पर चल पड़े। उस अग्निपथ को पार करते हुए वे दोनों शाम से पहले एक बस्ती में पहुंचे महेन्द्र को मन ही मन आशा थी कि बस्ती में पहुंचकर पत्नी व बच्ची के मुंह में शीतल जल दे सकेंगे, प्राण-रक्षा के लिए दो कौर भी नसीब होंगे। लेकिन कहां ? बस्ती में तो एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। बड़े-बड़े घरों में सन्नाटा छाया हुआ था, सारे लोग वहां से भाग चुके थे। महेन्द्र ने इधर-उधर देखने के बाद बच्ची को एक मकान में ले जाकर लिटा दिया। बाहर आकर वे ऊंचे स्वर में बुलाने पुकारने लगे। मगर उन्हें कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला।
वे कल्याणी से बोले, ‘‘सुनो, तुम जरा हिम्मत बांधकर यहां अकेली बैठो यहां अगर गाय हुई तो श्रीकृष्ण की दया से मैं दूध ला रहा हूं।’’
यह कहकर उन्होंने मिट्टी की एक कलसी उठाई और घर से बाहर निकले। वहां कई कलसियां पड़ी थीं।
द्वितीय परिच्छेद
महेन्द्र चले गए।
कल्याणी अकेली बच्ची के साथ उस जनशून्य में लगभग अंधकारमय घर में बैठी
चारों ओर देख रही थी। मन ही मन उसे बेहद डर लग रहा था। कोई भी कहीं नजर
नहीं आ रहा था, किसी मानव का स्वर तक सुनायी नहीं पड़ रहा था, सिर्फ सियार
व कुत्तों का स्वर गूंज रहा था।
सोच रही थी, उन्हें क्यों जाने दिया, अच्छा तो यही था कुछ देर तक और भूख-प्यास बर्दाश्त कर लेती। जी में आया, चारों तरफ के दरवाजे बंद करके बैठे। मगर एक भी दरवाजे पर कपाट अथवा अर्गला नहीं थी। इस प्रकार चारों ओर निहारते-निहारते सामने के दरवाजे पर उसे एक छाया-सी नजर आयी। वह छाया मनुष्याकृति-सी प्रतीत हुई, पर ठीक मनुष्य-सी भी नहीं लगी। अतिशय शुष्क शीर्ण, अतिशय कृष्णवर्ण, नग्न, विकटाकर मनुष्य जैसा न जाने कब आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया था। कुछ क्षणों के बाद उसी छाया ने जैसे अपना एक हाथ उठाया। अस्ति-चर्म से आवण्टित, अति दीर्घ शुष्क हाथ की दीर्घ शुष्क उंगली से उसने जैसे किसी को इशारा किया।
कल्याणी के प्राण सूख गए। तभी उसी की तरह एक और छाया-शुष्क, कृष्णवर्ण, दीर्घाकार, नग्न-पहली छाया के बगल में आकर खड़ी हुई। उसके बाद एक और छाया आयी। इसके बाद एक और छाया। फिर कई छायाएं आ गयीं-धीरे-धीरे चुपचाप वे सब कमरे में एकत्र हो गयीं। वह लगभग अंधकारमय घर रात के शमशान की तरह भयावह हो उठा। तभी वे सारी प्रेतवत मूर्तियां कल्याणी व उसकी बच्ची को घेरकर हो गयीं। कल्याणी लगभग मूर्च्छित-सी हो गयी।
अब कृष्णवर्ण शीर्ण छायाओं ने कल्याणी व उसकी बच्ची को पकड़ कर उठा लिया, फिर वे घर से बाहर निकलीं और मैदान को पार करते हुए जंगल में प्रवेश कर गयीं। कुछ क्षणों के बाद महेन्द्र कलसी में दूध लिए वहां आ पहुंचे। देखा, कोई कहीं नहीं। उन्होंने इधर-उधर खोजबीन की, बच्ची का नाम लेकर पुकारा, आखिर में पत्नी का कई बार नाम पुकारा, मगर कोई उत्तर नहीं मिला।
बच्ची व पत्नी का आसपास कोई चिह्न नहीं था।
सोच रही थी, उन्हें क्यों जाने दिया, अच्छा तो यही था कुछ देर तक और भूख-प्यास बर्दाश्त कर लेती। जी में आया, चारों तरफ के दरवाजे बंद करके बैठे। मगर एक भी दरवाजे पर कपाट अथवा अर्गला नहीं थी। इस प्रकार चारों ओर निहारते-निहारते सामने के दरवाजे पर उसे एक छाया-सी नजर आयी। वह छाया मनुष्याकृति-सी प्रतीत हुई, पर ठीक मनुष्य-सी भी नहीं लगी। अतिशय शुष्क शीर्ण, अतिशय कृष्णवर्ण, नग्न, विकटाकर मनुष्य जैसा न जाने कब आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया था। कुछ क्षणों के बाद उसी छाया ने जैसे अपना एक हाथ उठाया। अस्ति-चर्म से आवण्टित, अति दीर्घ शुष्क हाथ की दीर्घ शुष्क उंगली से उसने जैसे किसी को इशारा किया।
कल्याणी के प्राण सूख गए। तभी उसी की तरह एक और छाया-शुष्क, कृष्णवर्ण, दीर्घाकार, नग्न-पहली छाया के बगल में आकर खड़ी हुई। उसके बाद एक और छाया आयी। इसके बाद एक और छाया। फिर कई छायाएं आ गयीं-धीरे-धीरे चुपचाप वे सब कमरे में एकत्र हो गयीं। वह लगभग अंधकारमय घर रात के शमशान की तरह भयावह हो उठा। तभी वे सारी प्रेतवत मूर्तियां कल्याणी व उसकी बच्ची को घेरकर हो गयीं। कल्याणी लगभग मूर्च्छित-सी हो गयी।
अब कृष्णवर्ण शीर्ण छायाओं ने कल्याणी व उसकी बच्ची को पकड़ कर उठा लिया, फिर वे घर से बाहर निकलीं और मैदान को पार करते हुए जंगल में प्रवेश कर गयीं। कुछ क्षणों के बाद महेन्द्र कलसी में दूध लिए वहां आ पहुंचे। देखा, कोई कहीं नहीं। उन्होंने इधर-उधर खोजबीन की, बच्ची का नाम लेकर पुकारा, आखिर में पत्नी का कई बार नाम पुकारा, मगर कोई उत्तर नहीं मिला।
बच्ची व पत्नी का आसपास कोई चिह्न नहीं था।
तृतीय परिच्छेद
जिस वन में डाकू कल्याणी को ले आए, वह वन
बेहद मनोरम था। वहां रोशनी नहीं
थी, और न ही ऐसी आंखे थीं, जो वहां की शोभा देख पातीं, दरिद्र के हृदय में
छिपे सौंदर्य की भांति उस वन का सौंदर्य भी अगोचर था। देश में भले ही आहार
हो या न हो, वन में फूलों का अभाव नहीं था, फूलों की गंध ऐसी जबरदस्त कि
रोशनी का अभाव भी न खले। बीच में साफ सुकोमल चम्पा से घिरी जमीन के टुकड़े
पर डाकुओं ने कल्याणी और उसकी बच्ची को उतार दिया। वे सब उन दोनों को घेर
कर बैठ गये। इसके बाद वे लोग तर्क-वितर्क करने लगे कि इन दोनों का क्या
किया जाए ? जो अंलकार कल्याणी ने पहन रखे थे, वे सब पहले ही इन लोगों ने
हथिया लिए थे। डाकुओं का एक दल आभूषणों के बंटवारे में व्यस्त था।
जब आभूषण बंट गए तो एक डाकू बोला, ‘‘हम सोना-चांदी लेकर क्या करेंगे ? कोई एक गहना लेकर मुझे एक मुट्ठी चावल दे दे, बस भूख के मारे जान निकल रही है। आज सिर्फ पेड़ के पत्ते ही खाने को मिले हैं।’’
एक ने यह कहा तो सभी इसी तरह की बातें करने लगे। ‘‘चावल दो’’
‘‘चावल दो’’,‘‘भूख के मारे जान जा रही है’’, ‘‘सोना चांदी हमें नहीं चाहिए।’’
दल का सरदार उन्हें शांत करता हुआ कुछ बोला, मगर किसी ने एक नहीं सुनी, आपस में ही मार-पीट की नौबत आन पहुंची। जिन लोगों ने गहनें हथिया लिए थे, वे सब गुस्से से गहने फेंक-फेंक कर दल के सरदार को मारने लगे। दल के सरदार ने दो-एक को पकड़ कर पीटा, इस पर सबने मिलकर दल के सरदार पर हमला बोलकर उसे मारा-पीटा। दल का सरदार बिना-खाए पिए शीर्ण व अधमरा हो गया था, दो-एक चोटें लगते ही वह जमीन पर आ गिरा, और प्राण-त्याग कर दिए। इसके बाद भूखे, नाराज, उत्तेजित, ज्ञानशून्य डाकुओं के दल में एक बोला, ‘‘सियार और कुत्ते का माँस खा लिया, भूख के मारे जान जा रही है, आओ भाइयो, आज इसी साले को खाते हैं।’’
इस पर सबने ‘‘जय माँ काली’’ का नारा लगाकर घोष किया।
‘‘बम काली ! आज तो नरमाँस खाएंगे।’’ यह कहकर कमजोर शरीर के कृषकाय प्रेतवत समस्त डाकू अंधकार में खिलखिलाकर अट्टाहास कर उठे। ताली बजा-बजाकर नाचने लगे। दल के सरदार को जलाने के वास्ते एक डाकू अग्नि जलाने को प्रवृत्त हुआ। उसने सूखी लताएं, लड़कियां, घास-फूस एकत्र करके चकमक से आग प्रज्वलित की, तो एकत्र ढेर जल उठा। धीरे-धीरे आग तेजी पकड़ने लगी और आसपास के आम, जामुन, खजूर, पनस और बबूल आदि के पेड़ भी धीरे-धीरे आग पकड़ने लगे। कहीं आग में पत्ते जलने लगे, कहीं घास। कहीं अंधकार और हाढ़ा होने लगा। आग जल पड़ी तो एक नेमृतक के पांव पकड़ कर उसे खींचा और आग में झोंक दिया।
एक बोला, ‘‘ठहरो, ठहरो, अगर आज महा माँस खाने का इरादा किया ही है तो इस बूढ़े का सूखा माँस क्यों खाएं ? आज जो लूटकर लाए हैं, वहीं क्यों न खाएं। आओ, इस कोमल बच्ची को पकाकर खाएं।’’
इस पर सभी लोलुप होकर, जहां कल्याणी बच्ची को लेकर लेटी हुई थी, उसी तरफ देखने लगे। सबने देखा, अरे, वह जगह तो शून्य थी, बच्ची भी नहीं थी, उसकी माँ भी नहीं थी।
डाकुओं में जब वाद-विवाद चल रहा था, उस समय सुयोग पाकर कल्याणी बच्ची को गोद में लेकर व उसके मुंह को हथेली से भींचकर जंगल में कहीं भाग गयी थी।
शिकार को हाथ से निकलते देखकर ‘मारो’, ‘मारो’, का शोर मचाकर वे सारे डाकू चारों ओर दौड़ पड़े।
ऐसी दारुण स्थिति में पड़कर इंसान भी हिंसक पशु ही हो जाता है।
जब आभूषण बंट गए तो एक डाकू बोला, ‘‘हम सोना-चांदी लेकर क्या करेंगे ? कोई एक गहना लेकर मुझे एक मुट्ठी चावल दे दे, बस भूख के मारे जान निकल रही है। आज सिर्फ पेड़ के पत्ते ही खाने को मिले हैं।’’
एक ने यह कहा तो सभी इसी तरह की बातें करने लगे। ‘‘चावल दो’’
‘‘चावल दो’’,‘‘भूख के मारे जान जा रही है’’, ‘‘सोना चांदी हमें नहीं चाहिए।’’
दल का सरदार उन्हें शांत करता हुआ कुछ बोला, मगर किसी ने एक नहीं सुनी, आपस में ही मार-पीट की नौबत आन पहुंची। जिन लोगों ने गहनें हथिया लिए थे, वे सब गुस्से से गहने फेंक-फेंक कर दल के सरदार को मारने लगे। दल के सरदार ने दो-एक को पकड़ कर पीटा, इस पर सबने मिलकर दल के सरदार पर हमला बोलकर उसे मारा-पीटा। दल का सरदार बिना-खाए पिए शीर्ण व अधमरा हो गया था, दो-एक चोटें लगते ही वह जमीन पर आ गिरा, और प्राण-त्याग कर दिए। इसके बाद भूखे, नाराज, उत्तेजित, ज्ञानशून्य डाकुओं के दल में एक बोला, ‘‘सियार और कुत्ते का माँस खा लिया, भूख के मारे जान जा रही है, आओ भाइयो, आज इसी साले को खाते हैं।’’
इस पर सबने ‘‘जय माँ काली’’ का नारा लगाकर घोष किया।
‘‘बम काली ! आज तो नरमाँस खाएंगे।’’ यह कहकर कमजोर शरीर के कृषकाय प्रेतवत समस्त डाकू अंधकार में खिलखिलाकर अट्टाहास कर उठे। ताली बजा-बजाकर नाचने लगे। दल के सरदार को जलाने के वास्ते एक डाकू अग्नि जलाने को प्रवृत्त हुआ। उसने सूखी लताएं, लड़कियां, घास-फूस एकत्र करके चकमक से आग प्रज्वलित की, तो एकत्र ढेर जल उठा। धीरे-धीरे आग तेजी पकड़ने लगी और आसपास के आम, जामुन, खजूर, पनस और बबूल आदि के पेड़ भी धीरे-धीरे आग पकड़ने लगे। कहीं आग में पत्ते जलने लगे, कहीं घास। कहीं अंधकार और हाढ़ा होने लगा। आग जल पड़ी तो एक नेमृतक के पांव पकड़ कर उसे खींचा और आग में झोंक दिया।
एक बोला, ‘‘ठहरो, ठहरो, अगर आज महा माँस खाने का इरादा किया ही है तो इस बूढ़े का सूखा माँस क्यों खाएं ? आज जो लूटकर लाए हैं, वहीं क्यों न खाएं। आओ, इस कोमल बच्ची को पकाकर खाएं।’’
इस पर सभी लोलुप होकर, जहां कल्याणी बच्ची को लेकर लेटी हुई थी, उसी तरफ देखने लगे। सबने देखा, अरे, वह जगह तो शून्य थी, बच्ची भी नहीं थी, उसकी माँ भी नहीं थी।
डाकुओं में जब वाद-विवाद चल रहा था, उस समय सुयोग पाकर कल्याणी बच्ची को गोद में लेकर व उसके मुंह को हथेली से भींचकर जंगल में कहीं भाग गयी थी।
शिकार को हाथ से निकलते देखकर ‘मारो’, ‘मारो’, का शोर मचाकर वे सारे डाकू चारों ओर दौड़ पड़े।
ऐसी दारुण स्थिति में पड़कर इंसान भी हिंसक पशु ही हो जाता है।
चतुर्थ परिच्छेद
वन बेहद अंधकारमय था। कल्याणी को उसमें आगे
बढ़ने का मार्ग नहीं मिल रहा
था। वृक्षों-लताओं और झाड़-झंखाड़ों के घटाटोप में एक तो यों ही मार्ग
अवरुद्ध था, उस पर घना अंधेरा ! वृक्षों-लताओं और झाड़-झंखाड़ों को भेदकर
कल्याणी वन में प्रवेश करने लगी। बच्ची के शरीर में कांटे चुभ रहे थे।
बीच-बीच में रो उठती थी।रोने की आवाज सुनकर डाकू और भी चीखने-चिल्लाने लगे
थे। कल्याणी की देह भी कांटे चुभने से लहुलुहान हो गयी थी। इस प्रकार वह
वन में काफी दूर तक निकल आयी।
थोड़ी देर बाद चन्द्रोदय हुआ। अब तक कल्याणी को कुछ भरोसा था कि अंधकार में डाकू उसे देख नहीं पाएंगे, थोड़ी देर खोज-खाजकर वापस चले आएंगे, मगर चन्द्रोदय होते ही उसका यह भरोसा जाता रहा। चांद ने आकाश में उठकर वन के ऊपर आलोक बिखेर दिया-भीतर वन का अंधकार आलोक से भीग गया। अंधकार उज्ज्वल हो गया। जहां-तहां दरारों से छनकर आलोक वन में प्रवेश कर ताक-झांक करने लगा। चांद जितना ऊपर उठने लगा, उतना ही आलोक वन में प्रवेश करने लगा और सारा अंधकार वन में छिपने लगा। कल्याणी बच्ची को लेकर वन के अधिक अंदर चली गयी छिपने के लिए।
उधर डाकुओं का चीखना-चिल्लाना बढ़ गया था। वे चारों ओर से दौड़ते हुए चले आ रहे थे। बच्ची डर के मारे जोर-जोर से रोने लगी। कल्याणी हतोत्साहित हो गयी और भागने की कोशिश छोड़ दी। वह एक विशाल पेड़ के नीचे कंटकशून्य घास पर बैठ गयी। उसने बच्ची को गोद में बिठा लिया और पुकार-पुकार कर कहने लगी, ‘‘कहां हो तुम, जिसकी रोज मैं पूजा करती हूं, जिसका रोज मैं नमन करती हूं, जिसके भरोसे मैं इस वन में प्रवेश कर सकी, हे मधुसूदन, कहां हो तुमं ?’’
उसी समय भय, भक्ति की प्रगाढ़ता और क्षुधातृष्णा के अवसाद से कल्याणी धीरे-धीरे चेतनाशून्य हो गयी थी, मगर आंतरिक चेतना में उसे लगा, जैसे अंतरिक्ष में स्वर्गीय स्वर में गीत गाया जा रहा हो-
थोड़ी देर बाद चन्द्रोदय हुआ। अब तक कल्याणी को कुछ भरोसा था कि अंधकार में डाकू उसे देख नहीं पाएंगे, थोड़ी देर खोज-खाजकर वापस चले आएंगे, मगर चन्द्रोदय होते ही उसका यह भरोसा जाता रहा। चांद ने आकाश में उठकर वन के ऊपर आलोक बिखेर दिया-भीतर वन का अंधकार आलोक से भीग गया। अंधकार उज्ज्वल हो गया। जहां-तहां दरारों से छनकर आलोक वन में प्रवेश कर ताक-झांक करने लगा। चांद जितना ऊपर उठने लगा, उतना ही आलोक वन में प्रवेश करने लगा और सारा अंधकार वन में छिपने लगा। कल्याणी बच्ची को लेकर वन के अधिक अंदर चली गयी छिपने के लिए।
उधर डाकुओं का चीखना-चिल्लाना बढ़ गया था। वे चारों ओर से दौड़ते हुए चले आ रहे थे। बच्ची डर के मारे जोर-जोर से रोने लगी। कल्याणी हतोत्साहित हो गयी और भागने की कोशिश छोड़ दी। वह एक विशाल पेड़ के नीचे कंटकशून्य घास पर बैठ गयी। उसने बच्ची को गोद में बिठा लिया और पुकार-पुकार कर कहने लगी, ‘‘कहां हो तुम, जिसकी रोज मैं पूजा करती हूं, जिसका रोज मैं नमन करती हूं, जिसके भरोसे मैं इस वन में प्रवेश कर सकी, हे मधुसूदन, कहां हो तुमं ?’’
उसी समय भय, भक्ति की प्रगाढ़ता और क्षुधातृष्णा के अवसाद से कल्याणी धीरे-धीरे चेतनाशून्य हो गयी थी, मगर आंतरिक चेतना में उसे लगा, जैसे अंतरिक्ष में स्वर्गीय स्वर में गीत गाया जा रहा हो-
‘‘हरे मुरारे मधुकैटभारे।
गोपाल गोविंद मुकुन्द शौरे।
हरे मुरारे मधुकैटभारे।’’
कल्याणी ने बचपन में पुराणों में सुना था कि
देवर्षि गगन-पथ पर वीणा लेकर
हरिनाम का उच्चारण करते हुए भ्रमण करते रहते हैं, इस समय भी उसके मन में
यही दृष्य मूर्तिमान होने लगा। मन ही मन वह देख रही थीः शुभ्र-शरीर,
शुभ्र-केष, शुभ्र-दाढ़ी, शुभ्र-वसन, महा शरीर महामुनि हाथ में वीणा लिए
चंद्रलोक से प्रदीप्त नीले आकाश के पथ पर गा रहे हैं-
‘‘हरे मुरारे मधुकैटभारे।’’
क्रमशः गीत के बोल निकल आने लगे
और अधिक स्पष्ट सुनायी देने लगे-
‘‘हरे मुरारे मधुकैटभारे।’’
अन्त में कल्याणी के सिर के ऊपर वनस्थली को
गुंजाते हुए गीत के बोल फूटे-
‘‘हरे मुरारे मधुकैटभारे।’’
कल्याणी ने अपनी आंखें खोलीं। उस
अर्द्ध-स्फुट बनांधकार-मिश्रित
चंद्ररश्मियों में उसने देखा, सामने वही शुभ्र-शरीर, शुभ्र-केश,
शुभ्र-दाढ़ी शुभ्र-वसन वाली ऋषि-मूर्ति खड़ी है। अन्यमनस्क-सी खोयी-खोयी
कल्याणी को लगा, इन्हें प्रणाम करना चाहिए, मगर प्रणाम नहीं कर सकी। सिर
नवाते ही वह एकदम चेतनाशून्य होकर जमीन पर गिर पड़ी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book