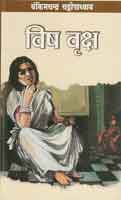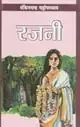|
नारी विमर्श >> विष वृक्ष विष वृक्षबंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय
|
355 पाठक हैं |
||||||
नारी की अंतर्वेदना पर आधारित उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय बंगला के शीर्षस्थ उपन्यासकार हैं। उनकी लेखनी से
बंगाल साहित्य तो समृद्ध हुआ ही है, हिन्दी भी उपकृत हुई है। उनकी
लोकप्रियता का यह आलम है कि पिछले डेढ़ सौ सालों से उनके उपन्यास विभिन्न
भाषाओं में अनूदित हो रहे हैं और कई-कई संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। उनके
उपन्यासों में नारी की अन्तर्वेदना व उसकी शक्तिमत्ता बेहद प्रभावशाली ढंग
से अभिव्यक्त हुई है। उनके उपन्यासों में नारी की गरिमा को नयी पहचान मिली
है और भारतीय इतिहास को समझने की नयी दृष्टि।
वे ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे। वे भारत के एलेक्जेंडर ड्यूमा माने जाते हैं।
कुंद ने बहुत दूर ऊपर काल-रहित अनन्त अपरिज्ञात नक्षत्र-लोक को देखकर कहा, ‘‘मैं इतना दूर नहीं चल पाऊंगी, मां। मुझमें बल नहीं।’’
यह सुनते ही कुंद की मां के कारुणिक चेहरे पर गंभीरता छा गई, किंचित रोष, मगर मृदु स्वर में बोली, ‘बेटी, जो तुम्हारी इच्छा हो, वही करो। मेरे साथ चलती हो तो अच्छा करती हो। बाद में तुम उस नक्षत्र-लोक की तरफ देखकर वहां आने के लिए तड़पती रहोगी। मैं एक बार फिर तुम्हारे पास आऊंगी। जब तुम मनः पीड़ा से व्याकुल होकर मुझे याद करोगी और मेरे साथ चलने को रोओगी, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तब तुम मेरे साथ चल पड़ना। इस समय तुम ऊपर ताक कर देखो, जहां मैं उंगली से इशारा कर रही हूं। वहां तुम्हें दो मानव-मूर्तियां नजर आएंगी। यही दो मानव इहलोक में तुम्हारे शुभ-अशुभ का कारण बनेंगे। यदि हो सके तो देखते ही उन्हें विषघर मानकर उनसे दूर भाग जाना। वे दोनों जिस राह से जाएं, उस राह से मत जाना।’’
वे ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे। वे भारत के एलेक्जेंडर ड्यूमा माने जाते हैं।
कुंद ने बहुत दूर ऊपर काल-रहित अनन्त अपरिज्ञात नक्षत्र-लोक को देखकर कहा, ‘‘मैं इतना दूर नहीं चल पाऊंगी, मां। मुझमें बल नहीं।’’
यह सुनते ही कुंद की मां के कारुणिक चेहरे पर गंभीरता छा गई, किंचित रोष, मगर मृदु स्वर में बोली, ‘बेटी, जो तुम्हारी इच्छा हो, वही करो। मेरे साथ चलती हो तो अच्छा करती हो। बाद में तुम उस नक्षत्र-लोक की तरफ देखकर वहां आने के लिए तड़पती रहोगी। मैं एक बार फिर तुम्हारे पास आऊंगी। जब तुम मनः पीड़ा से व्याकुल होकर मुझे याद करोगी और मेरे साथ चलने को रोओगी, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तब तुम मेरे साथ चल पड़ना। इस समय तुम ऊपर ताक कर देखो, जहां मैं उंगली से इशारा कर रही हूं। वहां तुम्हें दो मानव-मूर्तियां नजर आएंगी। यही दो मानव इहलोक में तुम्हारे शुभ-अशुभ का कारण बनेंगे। यदि हो सके तो देखते ही उन्हें विषघर मानकर उनसे दूर भाग जाना। वे दोनों जिस राह से जाएं, उस राह से मत जाना।’’
विष वृक्ष
प्रथम परिच्छेद
नगेन्द्र की नौका यात्रा
नगेन्द्र दत्त नाव पर सवार होकर सफर कर रहे थे। ज्येष्ठ का महीना था।
तूफान का महीना। पत्नी सूर्यमुखी ने सिर की कसम देकर कहा था,
‘‘सुनो, सावधान होकर नाव ले जाना। तूफान की संभावना
देखो तो
नाव को नदी किनारे बांध देना। बारिश–तूफान में कभी भी नाव में
मत
रहना।’’
नगेन्द्र ने यह सब मान लिया था, तभी सूर्यमुखी ने उन्हें नाव में सवार होने की स्वीकृति दी थी। कलकत्ता जाना भी बहुत जरूरी था, वहां जाकर महत्त्वपूर्ण काम निपटाने थे।
नगेन्द्र दत्त बेहद धनवान थे। विशाल जमींदारी उनकी थी। गोविंदपुर में थे। जिस जिले में यह गांव पड़ता था, उसका वास्तविक नाम गुप्त रखकर हम उसका उल्लेख हरिपुर के नाम से करेंगे।
नगेन्द्र बाबू युवा थे, अभी सिर्फ तीस साल ही हुए थे। नगेन्द्र दत्त अपने बजरे से सफर कर रहे थे। शुरु के दो दिन निर्विघ्न गुजर गए। नगेन्द्र की आँखें लगातार नदी के पानी को निहार रही थीं—जो अविरल कल-कल कहता बह रहा था, इठला रहा था, हवा में नाच रहा था, धूप में हंस रहा था, आवर्तों में गूंज रहा था। पानी अशांत था, अनन्त था और क्रीड़ामय। नदी के किनारे तटों पर, मैदानों में चरवाहे गाएं चरा रहे थे, कुछ वृक्षों के नीचे बैठे गा रहे थे, कुछ हुक्का गुड़ गुड़ा रहे थे, कुछ मारामारी कर रहे थे तो कुछ चना-चबेना खा रहे थे। किसान खेतों को सींच रहे थे, गायों को भगा रहे थे। घाट-घाट पर किसानों की बीवियां विराजमान थीं, हाथों में कलसियां, गले में चांदी के ताबीज, नाक के नथ, शरीर पर दो महीनों के मैलेकपड़े, स्याही से भी अधिक काले चेहरे, रूखे-सूखे बाल। उनके बीच कोई सुन्दरी सिर पर मिट्टी मलकर बाल धो रही थी, कोई बच्चे को नहला रही थी तो कोई पड़ोसिन से लड़-झगड़ रही थी। कुछ औरतें कपड़े सुखाती नजर आ रही थीं। कहीं-कहीं भले गांव के घाट पर कुल-कामनियां घाट को आलोकित कर रही थीं। बूढ़ी औरतें गपशप में लगी हुई थीं। प्रौढ़ाएँ शिव-पूजा कर रही थीं।
नव-युवतियां घूंघट ओढ़े पानी में डुबकी लगी रही थीं उनके बाल-बच्चे किनारे पर शोर मचा रहे थे, कीचड़ से खेल रहे थे, पूजा के फूल नोच रहे थे, तैर रहे थे, दूसरों के ऊपर पानी उलीच रहे थे, कभी-कभी ध्यानमग्न आंखें मींचे किसी गृहणी के सामने रखा मिट्टी का बना शिव उठाकर भाग जाते। ब्राह्मण-ठाकुर निरीह व भले मानुष की तरह मन-ही-मन गंगास्तव पढ़ रहे थे, पूजा कर रहे थे और बीच-बीच में आस-पास नहा रही युवतियों को कनखियों से देख रहे थे।
आकाश में सफेद बादल धूप से तप्त होकर भागे जा रहे थे, उनके बीच काले बिंदुओं-से पक्षी उड़ रहे थे। नारियल के पेड़ पर बैठी चील राजमंत्री की तरह चारों तरफ देख रही थी। इधर-उधर कई छोटी-छोटी चिड़ियां उड़ रही थीं। हाठ की नौकाएं अपनी ही धुन में आगे बढ़ती जा रही थीं। कई नौकाएं थीं, जो या तो चल रही थीं या किनारे पर खड़ी थीं।
शुरू के दो-एक दिन नागेन्द्र यह सब देखते रहे। बाद में एक दिन आकाश में घने बादल छा गए। बादलों से आकाश ढंक गया। नदी का पानी काला हो गया पेड़ खामोश हो गए, बत्तखें उड़ गईं। नदी निष्पन्द पड़ गई।
नगेन्द्र ने नाविकों को आदेश दिया, ‘‘नाव को किनारे से बांध दो।’’
रहमत मौला मल्लाह उस समय नमाज पढ़ रहा था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रहमत ने कभी पहले मल्लाहगिरी नहीं की थी। उसके नाना की खाला मल्लाह की बेटी थी, इसी पृष्ठ भूमि के बल पर वह मल्लाहगिरी की उम्मीदवारी में खड़ा हुआ था और सौभाग्य से चुन लिया गया था। रहमत जवाब देने में कोताही नहीं करता था। नमाज खत्म करने के बाद बाबू की ओर देखकर बोला, ‘‘डरने की कोई बात नहीं हुजूर ! आप निश्चिंत रहिए।’’
रहमत की इस निडरता का एक ही कारण था, वह यह कि किनारा बहुत पास था। जल्द ही नाव किनारे से आ लगी। नाविकों ने नीचे उतरकर नाव बांध दी।
लगता है, रहमत मौला देवता कुछ नाराज थे। हवा आगे बढ़ आई। हवा कुछ देर तक पेड़ों के पत्तों व डालियों से मल्लयुद्ध करती रही, फिर अपनी सहोदर वर्षा को बला लाई। इसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर खूब उत्पात मचाया। बहन वर्षा, बहन हवा के कन्धे पर सवार होकर उड़ने लगी। दोनों बहनें पेड़ों का सिर पकड़कर खूब हिलातीं, डालियां तोड़तीं, लताएं नोचतीं, फूल तहस-नहस करतीं, नदी का पानी उछालती और जो जी में आता, कहर बरपातीं। एक बहन रहमत मौला की टोपी उड़ा ले गई तो दूसरी बहन ने दाढ़ी को जलधारा के रूप में बदल दिया। पतवार चलाने वालों ने पाल नीचे उतार लिया। नौकर-चाकर नाव की सार-संभाल में लग गए।
नगेन्द्र संकट में फंस गए। आंधी-वर्षा के डर से अगर नाव से उतरते हैं तो नाविक उन्हें डरपोक समझेंगे, नहीं उतरते हैं तो सूर्यमुखी के सामने झूठा बनना पड़ेगा। आप लोगों में से कई पाठक पूछ सकते हैं कि उतरने में नुकसान ही कैसा ? हमें इसका पता नहीं, मगर नगेन्द्र को इसमें नुकसान नजर आता था। ऐसे समय में रहमत ने उन्हें संकट से उबार लिया। बोला हुजूर, पुराना मल्लाह हूं, न जाने आगे क्या हो, आंधी-पानी बढ़ता ही जा रहा है, नाव से उतरना ही बेहतर है।’’
नगेन्द्र चुपचाप नाव से उतर पड़े।
नदी किनारे आंधी-पानी में निराश्रय खड़ा रहना किसी के लिए भी आसान नहीं। शाम हो गई, पर आंधी-पानी ने थमने का नाम नहीं लिया। अब नगेन्द्र ने कोई आश्रय खोजना जरूरी समझा। सो वे गांव की ओर चल पड़े। नदी से गांव कुछ दूर था नगेन्द्र कीचड़-सने रास्ते पर पैदल ही जा रहे थे। इस बीच वर्षा भी थम गई, आंधी भी। मगर आकाश में अभी तक घने बादल छाए हुए थे, रात को जब दोबारा वर्षा होने की पूरी संभावना थी, सो नगेन्द्र आगे ही चलते रहे, वापस नहीं लौटे।
आकाश में काले बादल होने के कारण रात होने से पहले ही चारों ओर तक घनघोर अंधकार छा गया। गांव, घर, मैदान, रास्ते आदि कुछ नजर नहीं आ रहे थे। वातावरण में चारों तरफ जंगली पेड़े-पौधे फैले हुए थे। बीच-बीच में गर्जन-रहित बादलों में बिजली कौंध पड़ती थी। अभी-अभी खत्म हुई वर्षा से प्रसन्न होकर मेढक खूब शोर मचा रहे थे। झींगुरों का स्वर बहुत मद्धिम था, जो खास ध्यान लगाकर ही सुना जा सकता था। इन स्वरों के अलावा सुनाई पड़ रहा था, वृक्ष के पत्तों पर टपकती बूंदों का स्वर और उन बूंदों के धरती पर गिरने का स्वर, जल भरे रास्तों पर सियारों की पदचाप तथा वृक्षों पर बैठे पक्षियों के पंख फड़फड़ाने का स्वर। कभी-कभी थमी हुई हवा में तनिक तेजी आ जाती, जिससे वृक्ष के पत्तों पर अटकी बूंदें एक साथ धरती पर आ गिरती।
एकाएक नगेन्द्र ने दूर रोशनी की झलक देखी। उन्होंने देर करना उचित न समझा, जल-प्लावित धरती को पार करते हुए, पेड़ों से टपकती बूँदों से भीतरे हुए और सियारों को डराते-धमकाते हुए, वे उसी रोशनी की ओर बढ़ते चले गए। बहुत कष्ट सहकर आखिर कार रोशनी के पास आ पहुंचे। देखा, ईंटों से बने एक पुराने घर से रोशनी निकल रही है। घर का दरवाजा खुला हुआ था। नगेन्द्र ने नौकर को बाहर ही रुकने का इशारा किया और खुद अन्दर चले गए। देखा घर की स्थिति भयानक है।
नगेन्द्र ने यह सब मान लिया था, तभी सूर्यमुखी ने उन्हें नाव में सवार होने की स्वीकृति दी थी। कलकत्ता जाना भी बहुत जरूरी था, वहां जाकर महत्त्वपूर्ण काम निपटाने थे।
नगेन्द्र दत्त बेहद धनवान थे। विशाल जमींदारी उनकी थी। गोविंदपुर में थे। जिस जिले में यह गांव पड़ता था, उसका वास्तविक नाम गुप्त रखकर हम उसका उल्लेख हरिपुर के नाम से करेंगे।
नगेन्द्र बाबू युवा थे, अभी सिर्फ तीस साल ही हुए थे। नगेन्द्र दत्त अपने बजरे से सफर कर रहे थे। शुरु के दो दिन निर्विघ्न गुजर गए। नगेन्द्र की आँखें लगातार नदी के पानी को निहार रही थीं—जो अविरल कल-कल कहता बह रहा था, इठला रहा था, हवा में नाच रहा था, धूप में हंस रहा था, आवर्तों में गूंज रहा था। पानी अशांत था, अनन्त था और क्रीड़ामय। नदी के किनारे तटों पर, मैदानों में चरवाहे गाएं चरा रहे थे, कुछ वृक्षों के नीचे बैठे गा रहे थे, कुछ हुक्का गुड़ गुड़ा रहे थे, कुछ मारामारी कर रहे थे तो कुछ चना-चबेना खा रहे थे। किसान खेतों को सींच रहे थे, गायों को भगा रहे थे। घाट-घाट पर किसानों की बीवियां विराजमान थीं, हाथों में कलसियां, गले में चांदी के ताबीज, नाक के नथ, शरीर पर दो महीनों के मैलेकपड़े, स्याही से भी अधिक काले चेहरे, रूखे-सूखे बाल। उनके बीच कोई सुन्दरी सिर पर मिट्टी मलकर बाल धो रही थी, कोई बच्चे को नहला रही थी तो कोई पड़ोसिन से लड़-झगड़ रही थी। कुछ औरतें कपड़े सुखाती नजर आ रही थीं। कहीं-कहीं भले गांव के घाट पर कुल-कामनियां घाट को आलोकित कर रही थीं। बूढ़ी औरतें गपशप में लगी हुई थीं। प्रौढ़ाएँ शिव-पूजा कर रही थीं।
नव-युवतियां घूंघट ओढ़े पानी में डुबकी लगी रही थीं उनके बाल-बच्चे किनारे पर शोर मचा रहे थे, कीचड़ से खेल रहे थे, पूजा के फूल नोच रहे थे, तैर रहे थे, दूसरों के ऊपर पानी उलीच रहे थे, कभी-कभी ध्यानमग्न आंखें मींचे किसी गृहणी के सामने रखा मिट्टी का बना शिव उठाकर भाग जाते। ब्राह्मण-ठाकुर निरीह व भले मानुष की तरह मन-ही-मन गंगास्तव पढ़ रहे थे, पूजा कर रहे थे और बीच-बीच में आस-पास नहा रही युवतियों को कनखियों से देख रहे थे।
आकाश में सफेद बादल धूप से तप्त होकर भागे जा रहे थे, उनके बीच काले बिंदुओं-से पक्षी उड़ रहे थे। नारियल के पेड़ पर बैठी चील राजमंत्री की तरह चारों तरफ देख रही थी। इधर-उधर कई छोटी-छोटी चिड़ियां उड़ रही थीं। हाठ की नौकाएं अपनी ही धुन में आगे बढ़ती जा रही थीं। कई नौकाएं थीं, जो या तो चल रही थीं या किनारे पर खड़ी थीं।
शुरू के दो-एक दिन नागेन्द्र यह सब देखते रहे। बाद में एक दिन आकाश में घने बादल छा गए। बादलों से आकाश ढंक गया। नदी का पानी काला हो गया पेड़ खामोश हो गए, बत्तखें उड़ गईं। नदी निष्पन्द पड़ गई।
नगेन्द्र ने नाविकों को आदेश दिया, ‘‘नाव को किनारे से बांध दो।’’
रहमत मौला मल्लाह उस समय नमाज पढ़ रहा था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रहमत ने कभी पहले मल्लाहगिरी नहीं की थी। उसके नाना की खाला मल्लाह की बेटी थी, इसी पृष्ठ भूमि के बल पर वह मल्लाहगिरी की उम्मीदवारी में खड़ा हुआ था और सौभाग्य से चुन लिया गया था। रहमत जवाब देने में कोताही नहीं करता था। नमाज खत्म करने के बाद बाबू की ओर देखकर बोला, ‘‘डरने की कोई बात नहीं हुजूर ! आप निश्चिंत रहिए।’’
रहमत की इस निडरता का एक ही कारण था, वह यह कि किनारा बहुत पास था। जल्द ही नाव किनारे से आ लगी। नाविकों ने नीचे उतरकर नाव बांध दी।
लगता है, रहमत मौला देवता कुछ नाराज थे। हवा आगे बढ़ आई। हवा कुछ देर तक पेड़ों के पत्तों व डालियों से मल्लयुद्ध करती रही, फिर अपनी सहोदर वर्षा को बला लाई। इसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर खूब उत्पात मचाया। बहन वर्षा, बहन हवा के कन्धे पर सवार होकर उड़ने लगी। दोनों बहनें पेड़ों का सिर पकड़कर खूब हिलातीं, डालियां तोड़तीं, लताएं नोचतीं, फूल तहस-नहस करतीं, नदी का पानी उछालती और जो जी में आता, कहर बरपातीं। एक बहन रहमत मौला की टोपी उड़ा ले गई तो दूसरी बहन ने दाढ़ी को जलधारा के रूप में बदल दिया। पतवार चलाने वालों ने पाल नीचे उतार लिया। नौकर-चाकर नाव की सार-संभाल में लग गए।
नगेन्द्र संकट में फंस गए। आंधी-वर्षा के डर से अगर नाव से उतरते हैं तो नाविक उन्हें डरपोक समझेंगे, नहीं उतरते हैं तो सूर्यमुखी के सामने झूठा बनना पड़ेगा। आप लोगों में से कई पाठक पूछ सकते हैं कि उतरने में नुकसान ही कैसा ? हमें इसका पता नहीं, मगर नगेन्द्र को इसमें नुकसान नजर आता था। ऐसे समय में रहमत ने उन्हें संकट से उबार लिया। बोला हुजूर, पुराना मल्लाह हूं, न जाने आगे क्या हो, आंधी-पानी बढ़ता ही जा रहा है, नाव से उतरना ही बेहतर है।’’
नगेन्द्र चुपचाप नाव से उतर पड़े।
नदी किनारे आंधी-पानी में निराश्रय खड़ा रहना किसी के लिए भी आसान नहीं। शाम हो गई, पर आंधी-पानी ने थमने का नाम नहीं लिया। अब नगेन्द्र ने कोई आश्रय खोजना जरूरी समझा। सो वे गांव की ओर चल पड़े। नदी से गांव कुछ दूर था नगेन्द्र कीचड़-सने रास्ते पर पैदल ही जा रहे थे। इस बीच वर्षा भी थम गई, आंधी भी। मगर आकाश में अभी तक घने बादल छाए हुए थे, रात को जब दोबारा वर्षा होने की पूरी संभावना थी, सो नगेन्द्र आगे ही चलते रहे, वापस नहीं लौटे।
आकाश में काले बादल होने के कारण रात होने से पहले ही चारों ओर तक घनघोर अंधकार छा गया। गांव, घर, मैदान, रास्ते आदि कुछ नजर नहीं आ रहे थे। वातावरण में चारों तरफ जंगली पेड़े-पौधे फैले हुए थे। बीच-बीच में गर्जन-रहित बादलों में बिजली कौंध पड़ती थी। अभी-अभी खत्म हुई वर्षा से प्रसन्न होकर मेढक खूब शोर मचा रहे थे। झींगुरों का स्वर बहुत मद्धिम था, जो खास ध्यान लगाकर ही सुना जा सकता था। इन स्वरों के अलावा सुनाई पड़ रहा था, वृक्ष के पत्तों पर टपकती बूंदों का स्वर और उन बूंदों के धरती पर गिरने का स्वर, जल भरे रास्तों पर सियारों की पदचाप तथा वृक्षों पर बैठे पक्षियों के पंख फड़फड़ाने का स्वर। कभी-कभी थमी हुई हवा में तनिक तेजी आ जाती, जिससे वृक्ष के पत्तों पर अटकी बूंदें एक साथ धरती पर आ गिरती।
एकाएक नगेन्द्र ने दूर रोशनी की झलक देखी। उन्होंने देर करना उचित न समझा, जल-प्लावित धरती को पार करते हुए, पेड़ों से टपकती बूँदों से भीतरे हुए और सियारों को डराते-धमकाते हुए, वे उसी रोशनी की ओर बढ़ते चले गए। बहुत कष्ट सहकर आखिर कार रोशनी के पास आ पहुंचे। देखा, ईंटों से बने एक पुराने घर से रोशनी निकल रही है। घर का दरवाजा खुला हुआ था। नगेन्द्र ने नौकर को बाहर ही रुकने का इशारा किया और खुद अन्दर चले गए। देखा घर की स्थिति भयानक है।
द्वितीय परिच्छेद
दीप-निर्वाण
यह घर कोई मामूली घर नहीं था। मगर अब ऐश्वर्य व संपदा के निशान मिट चुके
थे। सारे कमरे-टूटे फूटे, गंदे और जन-विहीन थे। चारों तरफ सिर्फ चूहों,
उल्लुओं व कई अन्य तरह के कीड़ों-मकोड़ों का साम्राज्य था। केवल एक कमरे
में रोशनी जल रही थी। उस कमरे में नगेन्द्र ने प्रवेश किया। देखा, कमरे
में मानव-जीवनोपयोगी थोड़ी-सी सामग्री रखी हुई है, मगर उस सामग्री से भी
दारिद्रय टपक रहा था। दो-एक हंडिया —एक टूटा हुआ चूल्हा-तीन-चार
बर्तन, यही थे घर के अलंकार। काली दीवारें, कोनों में धूल, इधर-उधर
तिलचटटे, मकड़ियां, छिपकलियां और चूहे। एक फटे-पुराने बिस्तर पर एक बूढ़ा
लेटा हुआ था। देखते ही लगता था कि उसका अंतिम समय आ पहुंचा है। बुझी-बुझी
आंखें, तेज सांसें और कांपते होंठ। बिस्तर के पार्श्व में एक
ईंट पर
एक दीया जल रहा था। उसमें तेल कम ही रह गया था। बिस्तर पर पड़े इंसान का
भी यही हाल था। इस इंसान के ऊपर एक अन्य दीया प्रज्वलित
था—अनुपम
गोरी और स्निग्ध-ज्योति से परिपूर्ण सुन्दर बालिका।
तेल-विहीन रोशनी की वजह से या संभावित विरहशोक की चिंता में खोए रहने की वजह से बूढ़े व बालिका में से किसी ने भी नगेन्द्र को कमरे में आते नहीं देखा। नगेन्द्र दरवाजे पर खड़े होकर बूढ़े की कथा-व्यथा सुनने लगे। वे दोनों, बूढ़ा और बालिका, इस भीड़-भरे संसार में बिलकुल अकेले थे। एक समय था, जब इनके पास सम्पदा थी,। सगे-संबंधी और ढेर सारे नौकर-चाकर थे। पर चंचला लक्ष्मी की कृपा से उनका एक-एक करके सब कुछ चला गया। इस गरीबी से पीड़ित बेटे-बटियों का दिन-ब-दिन म्लान होता चेहरा देखकर गृहिणी पहले ही परलोक सिधार गई। बाकी सब तारे भी उस चांद के साथ धीरे-धीरे काल के गाल में समा गए। एक वंशधर पुत्र, मां की आंखों की मणि और पिता के बुढ़ापे का सहारा भी बाप के सामने से हमेशा के लिए उठ गया। कोई बचा नहीं रहा, सिवा इस बूढ़े और लोक-मनोहारी बालिका के, वही दोनों जनहीन जंगल से घिरे टूटे-फूटे मकान में रहने लगे। दोनों एक-दूसरे के सहारे। कुंदनन्दिनी की उम्र विवाह-योग्य हो चुकी थी।
तेल-विहीन रोशनी की वजह से या संभावित विरहशोक की चिंता में खोए रहने की वजह से बूढ़े व बालिका में से किसी ने भी नगेन्द्र को कमरे में आते नहीं देखा। नगेन्द्र दरवाजे पर खड़े होकर बूढ़े की कथा-व्यथा सुनने लगे। वे दोनों, बूढ़ा और बालिका, इस भीड़-भरे संसार में बिलकुल अकेले थे। एक समय था, जब इनके पास सम्पदा थी,। सगे-संबंधी और ढेर सारे नौकर-चाकर थे। पर चंचला लक्ष्मी की कृपा से उनका एक-एक करके सब कुछ चला गया। इस गरीबी से पीड़ित बेटे-बटियों का दिन-ब-दिन म्लान होता चेहरा देखकर गृहिणी पहले ही परलोक सिधार गई। बाकी सब तारे भी उस चांद के साथ धीरे-धीरे काल के गाल में समा गए। एक वंशधर पुत्र, मां की आंखों की मणि और पिता के बुढ़ापे का सहारा भी बाप के सामने से हमेशा के लिए उठ गया। कोई बचा नहीं रहा, सिवा इस बूढ़े और लोक-मनोहारी बालिका के, वही दोनों जनहीन जंगल से घिरे टूटे-फूटे मकान में रहने लगे। दोनों एक-दूसरे के सहारे। कुंदनन्दिनी की उम्र विवाह-योग्य हो चुकी थी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book