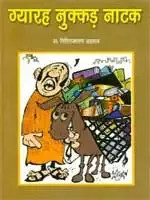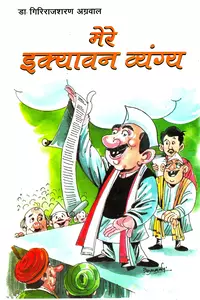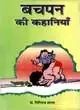|
नाटक-एकाँकी >> ग्यारह नुक्कड़ नाटक ग्यारह नुक्कड़ नाटकगिरिराजशरण अग्रवाल
|
414 पाठक हैं |
||||||
महँगाई,बेरोजगारी,बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रशासनिक एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार व प्रदूषण पर आधारित नुक्कड़ नाटक
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक उन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं,
जो नुक्कड़ नाटकों के लिए अनिवार्य हैं। इनमें सम्मिलित सभी नाटक ऐसे हैं,
जिन्हें सुव्यवस्थित मंच के बिना भी सीधे जनता के साथ जोड़ा जा सकता है।
अभाव, महँगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रशासनिक एवं राजनीतिक
भ्रष्टाचार, प्रदूषण आदि कितनी ही ऐसी समस्याएँ हैं जो सीधी जनजीवन से
जुड़ी हुई हैं और नुक्कड़ नाटक एक ऐसी सशक्त विधा है, जो जनसाधारण को
गहराई से और सीधे-सीधे अपने साथ जोड़ सकती है। ये नुक्कड़ नाटक अपने
उद्देश्य की पूर्ति सफलतापूर्वक करेंगे।
नुक्कड़, अभिनेता और हम दर्शक
जब मैं आपसे यह कहता हूँ कि मनुष्य धरती का पहला ऐसा प्राणी है, जो
अदाकारी कर सकता है, अभिनय कर सकता है तो मेरी बात का यह अभिप्राय भी है
कि यदि यह बात सत्य नहीं है तो कोई दूसरा प्राणी लाएँ, जो इतनी कुशलता के
साथ अनुकरण कर सकता हो। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। आप ऐसा
इसलिए नहीं कर सकेंगे कि अभिनय या अदाकारी के इतने गुण किसी और प्राणी में
हैं ही नहीं, जितने कि आदमी में हैं। यद्यपि थोड़ी-बहुत नाट्य कुशलता तो
प्रत्येक व्यक्ति में होती है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ-न-कुछ अदाकारी कर
सकता है, अभिनय कर सकता है; लेकिन जिनमें यह गुण असाधारण या उच्चतर का
होता है, वे इसे कला का रूप देकर अपनी इस क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन करने
में सफल हो जाते हैं।
आदमी कबसे अभिनय कर रहा है ? हज़ारों-लाखों वर्ष पुराने कलैंडर पर इसकी सही तिथि या काल को चिह्नित करना संभव नहीं है। लेकिन अब तक की खोज ने इस तथ्य को लगभग सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य ने अपने इतिहास के जिस प्रारंभिक काल में समूहों में एकत्र होकर रखना सीखा था, तभी से उसने नाट्यकला से अपना मनोरंजन करना भी सीख लिया था। गीत, नृत्य और नाट्य, ये तीन कलाएँ ऐसी हैं, जो आरंभ से मानव की सामूहिक गतिविधियों का केंद्र रही हैं। मनुष्यों के समूह दिन-भर के कड़े परिश्रम के बाद जब रात को निश्चित होकर मिल बैठते तो वे सामूहिक रूप से मनोरंजन की मुद्रा में गीत गाते, नृत्य करते या उन चीजों की नक़ल करके अपना मन बहलाते, जो उनके अनुभवों में आ चुकी होती थीं।
चित्रकला भी इतनी ही पुरानी है, जितनी मानव-सभ्यता। खुदाई में जो प्राचीन गुफाएँ मिली हैं, उसमें पशु-पक्षियों के चित्र ही नहीं मिले, अभिनय करते हुए मानव समूहों की चित्रकारी भी देखी गई है। मनुष्य की बुद्धि दूसरे समस्त प्राणियों की तुलना में अधिक तेज़ एवं कुशाग्र थी। वह गायन कर सकता था, नृत्य कर सकता था। दूसरे प्राणियों के लिए यह सब करना संभव नहीं था। आगे चलकर आदमी की इन कलात्मक प्रवृत्तियों ने मानव-सभ्यता को किस सीमा तक समृद्ध किया, इसका प्रमाण सभी ललित कलाओं के साथ-साथ नाट्यकला के निरंतर विकास में मिल सकता है। नाट्य कला ने मानव-समाज को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है। इसे विभिन्न शैलियों में रचा और विभिन्न रूपों में इसका प्रदर्शन किया जाता रहा।
नाट्यकला अपने विकास के प्रारंभिक काल में आदमी के सामान्य सामाजिक जीवन के साथ जुड़ने के अतिरिक्त उसकी धार्मिक गतिविधियों के साथ भी जुड़ी। कितने ही नाटक विभिन्न मानव-समुदायों की विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के आधार पर रचे और प्रदर्शित किए जाते रहे हैं। रामलीला, इंद्रसभा, कृष्णलीला, राजा हरिशचंद्र, खुदा दोस्त सुलतान किसने ही प्राचीन नाटक ऐसे हैं, जो शताब्दियों तक भारत के जनमानस की अभिरुचि तथा उसकी धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़े रहे और करोड़ों लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। आज भी गाँव-गाँव और शहर-शहर में इन नाटकों का प्रदर्शन होता है और आज भी असंख्य लोग इनसे भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि समय के साथ विकसित होती गई नाट्यकला को नियमित मंच तो बहुत बाद में मिला। आरम्भ में तो ये खुले मैदानों अथवा छायादार वृक्षों के नीचे पलती रही। नौटंकी हो या कठपुतली का तमाशा, रामलीला हो या खुदा दोस्त सुलतान की नाट्य-कथा, बिना सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित मंच के ही भारी जनसमूह के बीच इनका प्रदर्शन किया जाता रहा। इन्हें हम नाट्यकलाओं के प्रारंभिक रूप भी कह सकते हैं।
यह कहना ग़लत न होगा कि अन्य ललित कलाओं की तुलना में चाहे वह गीत हो या नृत्य, नाटक में अपने दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता अधिक है। क्योंकि जब आप कविता पढ़ रहे होते हैं या उसे सुन रहे होते हैं, तो आपके साथ बुद्धि, कान या आँखें ही संगत कर रही होती हैं, इसी तरह जब आप नृत्य देख रहे होते हैं तो बुद्धि और आँखें ही आपकी सहयोगी होती हैं। किंतु जब आप एक दर्शक के रूप में किसी नाटक में सम्मिलित होते हैं तो आपकी आँखें, कान अथवा यों कहिए कि आपकी समस्त इंद्रियाँ सक्रिय होकर उससे आनंदित होती हैं। यही नाट्यकला की श्रेष्ठता और विशेषता है।
जैसा कि ऊपर बताया गया है कि नाटक को एक सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित मंच तो बहुत बाद में मिला। प्रारंभ में तो यह गलियों, कूचों, मैदानों तथा छायादार वृक्षों के नीचे पलता रहा। इसी आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि अमंचीय नाटकों की इसी प्राचीन परंपरा ने आगे चलकर कुछ विशेष परिस्थितियों के परिणामस्वरूप नुक्कड़ नाटकों की परिपाटी को उभरने एवं विकसित होने में सहायता दी। आइए, इसका एक संक्षिप्त-सा अवलोकन करें।
साहित्य का इतिहास हमें बताता है कि शताब्दियों लंबी अवधि में नाट्यकला के जितने रूप हमारे सामने आए हैं, आरंभ में वे आदमी की मनोरंजनप्रियता तथा हास्य-विनोद की मौलिक प्रवृत्तियों से जन्मे थे। आज हम देखते हैं कि मंचीय नाटकों से लेकर, फ़िल्म के पर्दे पर दिखाए जाने वाले चलचित्रों, दूरदर्शन के स्क्रीन पर दिखाई जानेवाली नाट्य-गाथाओं, सीरियलों, आकाशवाणी से प्रसारित होनेवाले नाटकों तथा बस्तियों के भीड़-भरे स्थानों पर खेले जानेवाले नुक्कड़ नाटकों तक, इस कला के विभिन्न रूप हमारे सामने हैं। इसी के साथ-साथ प्राचीन ढंग की परंपरागत नौटंकियों के अतिरिक्त धार्मिक महत्त्व के नाट्य-प्रदर्शन भी अब तक हमारे समाज का अनिवार्य अंग बने हुए हैं। इन्होंने लोकप्रियता का ऐसा रिकार्ड बनाया है कि शायद ही ऐसा कोई उदाहरण मिल सके। दूरदर्शन पर दिखाए गए रामायण और महाभारत-जैसे नाटकों ने जिस गहराई से भारतीय जनमानस को प्रभावित किया, वह स्पष्ट रूप में इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक आस्थाओं से अलग हटकर भी नाट्यकला जनसाधारण को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करने की क्षमता रखती है, शर्त यह है कि वह कला की दृष्टि से उच्चकोटि की हो।
इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत में नाट्यकला का विकास वैदिककाल से ही आरंभ हो गया था। यह भी सर्वविदित है कि भरत-प्रणीत नाट्यशास्त्र नाट्यविधा का आदिग्रंथ माना जाता है। हम भारतीयों की आस्था है कि स्वयं ब्रह्मा ने ही नाट्यविधा को परिभाषित किया है। भारतवासियों की मान्यता है कि त्रेतायुग में देवताओं की प्रार्थाना पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद तथा आयुर्वेद के आधार पर पंचम वेद यानी नाट्यवेद की रचना की। इस वेद में चार अंग हैं-पाठ्य, गीत, अभिनय तथा रस।
इससे यह बात सहज ही समझी जा सकती है कि भारत में नाट्यकला की परंपरा कितनी पुरानी है। डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्रो. पिशेल आदि के मत से सहमति व्यक्त करते हुए लिखा है कि ऋग्वेद में पाए जानेवाले संवाद-सूत्र वास्तव में नाटक के प्रारंभिक अंश ही हैं। उक्त निष्कर्षों के आधार पर हम यह दावा तो कर ही सकते हैं कि वैदिक काल में नाट्यकला भले ही पूर्णरूप में विकसित एवं सुगठित न हुई हो, किंतु संवाद और कला-सामग्री के दृष्टिकोण से यह अपने लिए आधार अवश्य तैयार कर रही थी। यूरोपीय शोधकर्ता डा. रिजवे ने तो आदिमानव की पूजा-भावना के विभिन्न रूपों को भी नाट्यकला की प्रारंभिक स्थिति स्वीकार किया है। कुछ अन्य यूरोपीय विद्वानों जैसे प्रो. हिलेब्रां तथा प्रो. कोनो ने भी इस बात से सहमति व्यक्त की है कि नाट्यकला का उदय लौकिक कृत्यों के माध्यम से हुआ है। प्राचीन लोकसमाज में गाए जानेवाले गीतों, नृत्यों तथा मौसमों और उत्सवों में संपन्न होनेवाली विभिन्न गतिविधियों के गर्भ से ही नाटक ने जन्म लिया है। कठपुतली के खेल तथा छाया नाटकों से इस कला का प्राचीन संबंध है। जब हम नाट्यकला की प्राचीनता को खोजने के लिए निकलते हैं तो हमारा संपर्क सर्वप्रथम वैदिक काल की नाट्य-संबंधी सामग्री से ही होता है। इसी के साथ-साथ हमें लोकनाट्य-परंपरा के सूत्र भी आसानी से मिल जाते हैं।
लोकनाट्य-परंपरा के प्रमाण तो हमें सशक्त और स्पष्ट रूप में आठवीं-नवीं शताब्दी के इतिहास में मिलने आरंभ हो जाते हैं। हम देखते हैं कि भारत पर निरंतर होनेवाले विदेशी आक्रमणों के परिणामस्वरूप जो दवाब, दमन तथा अशांति की स्थिति समय-समय पर उत्पन्न होती रही, उसमें लोकनाट्य-परंपरा तेज़ी से विकसित हुई। इस कला के माध्यम से हास्य और व्यंग्य की शैली में जन-कलाकारों ने अपने क्रोध और विरोध को अभिव्यक्त किया। लेकिन तब तक नाट्य लोकविधा में कला का स्तर इतना सशक्त नहीं हुआ था, जितना बाद में हुआ। परिणामतः उस युग में कोई उल्लेखनीय नाटककार सामने नहीं आया। मुग़ल काल इस दृष्टिकोण से और भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसमें नाटक-लेखन अथवा नाटक-रचना लगभग रुक-सी गई। केवल जनमानस के आधार पर वही नाट्यसामग्री मंचित अथवा प्रदर्शित होती रही, जो पहले से उपलब्ध थी। इसी के साथ जब हम सामान्य लोकजीवन में झाँककर देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि अन्य लोककलाओं की भाँति नाट्यकला भी जनता के स्तर पर जीवित रही। इसे प्रमाणित करने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल में जात्रा, बिहार में विदेसिया, अवध की पूर्वी बोली, अवधी बोली ब्रज तथा खड़ीबोली में हमें जो रासरंग, स्वांग, नौटंकी, भांड और नक्काल देखने को मिलते हैं, वे इसी जननाट्य कला के विभिन्न रूप हैं, जो निरंतर भारतीय जनमानस के आकर्षण का कारण बने रहे।
लोकनाटक की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वह अपने लिए किसी सुव्यवस्थित मंच की माँग नहीं करता। वह आरंभ से ही मुक्त आकाश के नीचे अपने पाँव जमाता आया है। यह तो अपनी आवश्यकता के लिए अवसर के अनुसार अस्थाई मंच निर्मित करता है और उन अनिवार्यताओं से अपने-आपको बचा लेता है, जो स्थाई मंच के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। यह जननाटक पर्वों, धार्मिक उत्सवों एवं अनुष्ठानों के अवसरों पर खेले जाते रहे हैं और इनकी परंपरा बहुत पुरानी है।
आगे चलकर हमें हिंदी-नाटक का व्यवस्थित रूप दिखाई देता है। इसे हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारतेंदुयुग के नाम से परिभाषित कर सकते हैं। यद्यपि भारतेंदुयुग से पूर्व भी हिंदी-नाटक की मंचीय परंपरा विद्यमान है, भारतेंदु-पूर्व हिंदी-नाटकों की सूची में रस शैली के नाटक, संस्कृत प्रभाव वाले नाटक तथा अँग्रेज़ी नाटक के अनुवाद ही प्रमुख रूप से हमारे सामने आते हैं, लेकिन भारतेंदुयुग में इन्हें परिस्थितियों के अनुसार मोड़ा एवं विकसित किया गया। भारतेंदु ने सर्वप्रथम यह अनुभव किया कि भारतीय जनता को केवल संस्कृत परिपाटी पर आधारित नाटकों से संतुष्ट रखना समय के अनुकूल नहीं है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि पारसी रंगमंच भी भारतीय जनमानस की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा।
तब उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर नाटकों के लेखन तथा मंचन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतेंदु के उदय से हिंदी-नाट्य-कला को एक नई दिशा मिली। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि भारतेंदु न केवल आधुनिक हिंदी-नाटक के जन्मदाता हैं बल्कि समस्त हिंदी-साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के पुरोधा ऐतिहासिक महापुरुष हैं। उन्होंने और उनके समकालीन नाटककारों ने लीक से हटकर अपने-आपको समसामयिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के साथ जोड़ा तथा उद्देश्य को प्रमुखता देकर कलात्मक नाटकों, की रचना की। इन नाटककारों ने अपना ध्यान विशेष रूप में देश की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याओं की ओर केंद्रित किया। यह समय हिंदी-नाटक के लिए परिवर्तनशीलता का युग था।
पूरा देश उथल-पुथल से भरा हुआ था। यह वह समय था, जब एक ओर पुरातनवादी वर्ग अपनी सारी परंपराओं तथा रुढ़िवादी रीति-रिवाजों को ज्यों-का-त्यों बनाए रखने और उन्हें भारतीय संस्कृति का अपरिवर्तनीय आधार मानने की हठ कर रहा था तो दूसरा वर्ग प्राचीन परंपराओं एवं रूढ़ियों के बंधन से निकलकर पुनर्जागरण की ओर अग्रसर हो रहा था। ऐसी स्थिति में भारतेंदु हरिशचंद्र की दृष्टि नाट्यकला की ओर गई। क्योंकि यह कला अपनी प्राचीन परंपरा के कारण हास-परिहास अथवा मनोरंजन के दायरे से आगे नहीं निकल पा रही थी। इस नाट्य-परंपरा में कला और उद्देश्य दोनों का भारी अभाव था। इसके साथ ही रंगमंच की दशा भी शोचनीय थी। भारतेंदुयुग में यह गतिरोध टूटा और नाटक को उद्देश्यपूर्ण एवं संदर्भों के साथ जोड़कर एक व्यवस्थित रंगमंच दिया गया। इस युग में ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, राजनीतिक, रोमांटिक तथा राष्ट्रीयता प्रधान नाटक तो लिखे ही गए, साथ ही अच्छे और उच्चस्तरीय नाटकों का संस्कृत, बंगला तथा अँग्रेज़ी भाषाओं से अनुवाद भी किया गया।
यह घटना भी स्मरण कर लेनी चाहिए कि हिंदी-नाट्यकला का सबसे पहला रंगमंच काशी में 1868 में ‘बनारस थियेटर’ के नाम से स्थापित किया गया था। हिंदी-नाटक के विकास तथा रंगमंच की स्थापना की इसी पृष्ठभूमि में साहित्य के युगपुरुष जयशंकर प्रसाद का उदय हुआ। वे नाटक-रचयिता थे, अभिनेता नहीं थे। उन्होंने ऐतिहासिक विषयों से जुड़े सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले तथा भारतीय गौरव को दर्शाने वाले उच्चस्तरीय नाटक लिखे। हिंदी-नाटक को भारतेंदु ने जहाँ छोड़ा था, प्रसाद ने उसे आगे चलकर नया मोड़ दिया। प्रसाद ने हिंदी-नाटकों में ऐसे विषय भी जोड़े, जो उनसे पहले अमान्य अथवा अशोभनीय समझे जाते थे। उदाहरण के लिए हमें इन नाटकों में मंच पर ही युद्ध मृत्यु, हत्या, आत्महत्या, अपहरण, आदि-आदि के दृश्य भी दिखाई देते हैं। स्पष्ट है कि यह शैली पाश्चात्य परंपरा के प्रभाव से हिंदी-नाटकों में आई और इससे नाट्य-कला का क्षेत्र और विकसित हुआ।
यह सर्वविदित है कि भारतेंदु हरिशचंद्र के बाद का समय हिंदी-नाट्यकला के लिए विकास का उपयुक्त समय था। इस युग में गोविंदवल्लभ पंत, उग्र, सेठ गोविंददास हरिकृष्ण प्रेमी, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री तथा उदयशंकर भट्ट ने अच्छे मंचीय नाटक लिखे। इस युग में मौलिक नाटक भी लिखे गए। पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय व समस्या-प्रधान नाटक भी। इस युग में अच्छे नाटकों का विभिन्न भाषाओं से अनुवाद भी हुआ। लेकिन यह भी सही है कि जिस युग को हम ‘प्रसाद-युग’ का नाम देते हैं, वह रंगमंचीय दृष्टि से बहुत कम विकसित हुआ। प्रसाद-युग में या उसके उपरांत नाट्यकला के जिन रूपों का उदय हुआ, उनमें एकांकी की विधा अपना विशेष महत्त्व रखती है। यह एक नवीन तथा स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित भी हुई लोकप्रिय भी। एकांकी के साथ वे सारे विषय और समस्याएँ भी जुड़ गईं, जो अब तक नाट्यकला से दूर थीं।
एकांकी की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यह भी था कि इसमें समस्त आडंबरों को त्यागते हुए सामान्य जनजीवन और उससे जुड़ी समस्याओं को प्रस्तुत किया जाने लगा था। इन दैनिक समस्याओं में दर्शक अपने-आपको व्यक्तिगत रूप में सम्मिलित पाता था, जबकि पुराने राजा-महाराजाओं अथवा दैवीय घटनाओं पर रचित नाटकों से सामान्यजन की कोई संबद्धता नहीं होती थी। हिंदी में एकांकी नाटकों की रचना एवं प्रस्तुति यों तो भारतेंदु एवं द्विवेदी-युग में भी होती रही, किंतु उस समय ऐसा कोई लेखक या नाटककार उभरकर सामने नहीं आया, जो एकांकी रचना को नवीन शिल्प एवं कथा मापदंडों से जोड़ता। बाद में एकांकी को नया रूप, नई, तकनीक तथा प्रस्तुतिकरण का नया रंग-ढंग मिला।
देश की स्वतंत्रता के उपरांत हिंदी-एकांकी के विकास को और अधिक अनुकूल वातावरण मिला। उसके परिपक्व होने की संभावनाएँ और अधिक उज्ज्वल हुईं। इस प्रकार एकांकी एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित हो गया।
आदमी कबसे अभिनय कर रहा है ? हज़ारों-लाखों वर्ष पुराने कलैंडर पर इसकी सही तिथि या काल को चिह्नित करना संभव नहीं है। लेकिन अब तक की खोज ने इस तथ्य को लगभग सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य ने अपने इतिहास के जिस प्रारंभिक काल में समूहों में एकत्र होकर रखना सीखा था, तभी से उसने नाट्यकला से अपना मनोरंजन करना भी सीख लिया था। गीत, नृत्य और नाट्य, ये तीन कलाएँ ऐसी हैं, जो आरंभ से मानव की सामूहिक गतिविधियों का केंद्र रही हैं। मनुष्यों के समूह दिन-भर के कड़े परिश्रम के बाद जब रात को निश्चित होकर मिल बैठते तो वे सामूहिक रूप से मनोरंजन की मुद्रा में गीत गाते, नृत्य करते या उन चीजों की नक़ल करके अपना मन बहलाते, जो उनके अनुभवों में आ चुकी होती थीं।
चित्रकला भी इतनी ही पुरानी है, जितनी मानव-सभ्यता। खुदाई में जो प्राचीन गुफाएँ मिली हैं, उसमें पशु-पक्षियों के चित्र ही नहीं मिले, अभिनय करते हुए मानव समूहों की चित्रकारी भी देखी गई है। मनुष्य की बुद्धि दूसरे समस्त प्राणियों की तुलना में अधिक तेज़ एवं कुशाग्र थी। वह गायन कर सकता था, नृत्य कर सकता था। दूसरे प्राणियों के लिए यह सब करना संभव नहीं था। आगे चलकर आदमी की इन कलात्मक प्रवृत्तियों ने मानव-सभ्यता को किस सीमा तक समृद्ध किया, इसका प्रमाण सभी ललित कलाओं के साथ-साथ नाट्यकला के निरंतर विकास में मिल सकता है। नाट्य कला ने मानव-समाज को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है। इसे विभिन्न शैलियों में रचा और विभिन्न रूपों में इसका प्रदर्शन किया जाता रहा।
नाट्यकला अपने विकास के प्रारंभिक काल में आदमी के सामान्य सामाजिक जीवन के साथ जुड़ने के अतिरिक्त उसकी धार्मिक गतिविधियों के साथ भी जुड़ी। कितने ही नाटक विभिन्न मानव-समुदायों की विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के आधार पर रचे और प्रदर्शित किए जाते रहे हैं। रामलीला, इंद्रसभा, कृष्णलीला, राजा हरिशचंद्र, खुदा दोस्त सुलतान किसने ही प्राचीन नाटक ऐसे हैं, जो शताब्दियों तक भारत के जनमानस की अभिरुचि तथा उसकी धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़े रहे और करोड़ों लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। आज भी गाँव-गाँव और शहर-शहर में इन नाटकों का प्रदर्शन होता है और आज भी असंख्य लोग इनसे भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि समय के साथ विकसित होती गई नाट्यकला को नियमित मंच तो बहुत बाद में मिला। आरम्भ में तो ये खुले मैदानों अथवा छायादार वृक्षों के नीचे पलती रही। नौटंकी हो या कठपुतली का तमाशा, रामलीला हो या खुदा दोस्त सुलतान की नाट्य-कथा, बिना सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित मंच के ही भारी जनसमूह के बीच इनका प्रदर्शन किया जाता रहा। इन्हें हम नाट्यकलाओं के प्रारंभिक रूप भी कह सकते हैं।
यह कहना ग़लत न होगा कि अन्य ललित कलाओं की तुलना में चाहे वह गीत हो या नृत्य, नाटक में अपने दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता अधिक है। क्योंकि जब आप कविता पढ़ रहे होते हैं या उसे सुन रहे होते हैं, तो आपके साथ बुद्धि, कान या आँखें ही संगत कर रही होती हैं, इसी तरह जब आप नृत्य देख रहे होते हैं तो बुद्धि और आँखें ही आपकी सहयोगी होती हैं। किंतु जब आप एक दर्शक के रूप में किसी नाटक में सम्मिलित होते हैं तो आपकी आँखें, कान अथवा यों कहिए कि आपकी समस्त इंद्रियाँ सक्रिय होकर उससे आनंदित होती हैं। यही नाट्यकला की श्रेष्ठता और विशेषता है।
जैसा कि ऊपर बताया गया है कि नाटक को एक सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित मंच तो बहुत बाद में मिला। प्रारंभ में तो यह गलियों, कूचों, मैदानों तथा छायादार वृक्षों के नीचे पलता रहा। इसी आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि अमंचीय नाटकों की इसी प्राचीन परंपरा ने आगे चलकर कुछ विशेष परिस्थितियों के परिणामस्वरूप नुक्कड़ नाटकों की परिपाटी को उभरने एवं विकसित होने में सहायता दी। आइए, इसका एक संक्षिप्त-सा अवलोकन करें।
साहित्य का इतिहास हमें बताता है कि शताब्दियों लंबी अवधि में नाट्यकला के जितने रूप हमारे सामने आए हैं, आरंभ में वे आदमी की मनोरंजनप्रियता तथा हास्य-विनोद की मौलिक प्रवृत्तियों से जन्मे थे। आज हम देखते हैं कि मंचीय नाटकों से लेकर, फ़िल्म के पर्दे पर दिखाए जाने वाले चलचित्रों, दूरदर्शन के स्क्रीन पर दिखाई जानेवाली नाट्य-गाथाओं, सीरियलों, आकाशवाणी से प्रसारित होनेवाले नाटकों तथा बस्तियों के भीड़-भरे स्थानों पर खेले जानेवाले नुक्कड़ नाटकों तक, इस कला के विभिन्न रूप हमारे सामने हैं। इसी के साथ-साथ प्राचीन ढंग की परंपरागत नौटंकियों के अतिरिक्त धार्मिक महत्त्व के नाट्य-प्रदर्शन भी अब तक हमारे समाज का अनिवार्य अंग बने हुए हैं। इन्होंने लोकप्रियता का ऐसा रिकार्ड बनाया है कि शायद ही ऐसा कोई उदाहरण मिल सके। दूरदर्शन पर दिखाए गए रामायण और महाभारत-जैसे नाटकों ने जिस गहराई से भारतीय जनमानस को प्रभावित किया, वह स्पष्ट रूप में इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक आस्थाओं से अलग हटकर भी नाट्यकला जनसाधारण को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करने की क्षमता रखती है, शर्त यह है कि वह कला की दृष्टि से उच्चकोटि की हो।
इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत में नाट्यकला का विकास वैदिककाल से ही आरंभ हो गया था। यह भी सर्वविदित है कि भरत-प्रणीत नाट्यशास्त्र नाट्यविधा का आदिग्रंथ माना जाता है। हम भारतीयों की आस्था है कि स्वयं ब्रह्मा ने ही नाट्यविधा को परिभाषित किया है। भारतवासियों की मान्यता है कि त्रेतायुग में देवताओं की प्रार्थाना पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद तथा आयुर्वेद के आधार पर पंचम वेद यानी नाट्यवेद की रचना की। इस वेद में चार अंग हैं-पाठ्य, गीत, अभिनय तथा रस।
इससे यह बात सहज ही समझी जा सकती है कि भारत में नाट्यकला की परंपरा कितनी पुरानी है। डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्रो. पिशेल आदि के मत से सहमति व्यक्त करते हुए लिखा है कि ऋग्वेद में पाए जानेवाले संवाद-सूत्र वास्तव में नाटक के प्रारंभिक अंश ही हैं। उक्त निष्कर्षों के आधार पर हम यह दावा तो कर ही सकते हैं कि वैदिक काल में नाट्यकला भले ही पूर्णरूप में विकसित एवं सुगठित न हुई हो, किंतु संवाद और कला-सामग्री के दृष्टिकोण से यह अपने लिए आधार अवश्य तैयार कर रही थी। यूरोपीय शोधकर्ता डा. रिजवे ने तो आदिमानव की पूजा-भावना के विभिन्न रूपों को भी नाट्यकला की प्रारंभिक स्थिति स्वीकार किया है। कुछ अन्य यूरोपीय विद्वानों जैसे प्रो. हिलेब्रां तथा प्रो. कोनो ने भी इस बात से सहमति व्यक्त की है कि नाट्यकला का उदय लौकिक कृत्यों के माध्यम से हुआ है। प्राचीन लोकसमाज में गाए जानेवाले गीतों, नृत्यों तथा मौसमों और उत्सवों में संपन्न होनेवाली विभिन्न गतिविधियों के गर्भ से ही नाटक ने जन्म लिया है। कठपुतली के खेल तथा छाया नाटकों से इस कला का प्राचीन संबंध है। जब हम नाट्यकला की प्राचीनता को खोजने के लिए निकलते हैं तो हमारा संपर्क सर्वप्रथम वैदिक काल की नाट्य-संबंधी सामग्री से ही होता है। इसी के साथ-साथ हमें लोकनाट्य-परंपरा के सूत्र भी आसानी से मिल जाते हैं।
लोकनाट्य-परंपरा के प्रमाण तो हमें सशक्त और स्पष्ट रूप में आठवीं-नवीं शताब्दी के इतिहास में मिलने आरंभ हो जाते हैं। हम देखते हैं कि भारत पर निरंतर होनेवाले विदेशी आक्रमणों के परिणामस्वरूप जो दवाब, दमन तथा अशांति की स्थिति समय-समय पर उत्पन्न होती रही, उसमें लोकनाट्य-परंपरा तेज़ी से विकसित हुई। इस कला के माध्यम से हास्य और व्यंग्य की शैली में जन-कलाकारों ने अपने क्रोध और विरोध को अभिव्यक्त किया। लेकिन तब तक नाट्य लोकविधा में कला का स्तर इतना सशक्त नहीं हुआ था, जितना बाद में हुआ। परिणामतः उस युग में कोई उल्लेखनीय नाटककार सामने नहीं आया। मुग़ल काल इस दृष्टिकोण से और भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसमें नाटक-लेखन अथवा नाटक-रचना लगभग रुक-सी गई। केवल जनमानस के आधार पर वही नाट्यसामग्री मंचित अथवा प्रदर्शित होती रही, जो पहले से उपलब्ध थी। इसी के साथ जब हम सामान्य लोकजीवन में झाँककर देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि अन्य लोककलाओं की भाँति नाट्यकला भी जनता के स्तर पर जीवित रही। इसे प्रमाणित करने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल में जात्रा, बिहार में विदेसिया, अवध की पूर्वी बोली, अवधी बोली ब्रज तथा खड़ीबोली में हमें जो रासरंग, स्वांग, नौटंकी, भांड और नक्काल देखने को मिलते हैं, वे इसी जननाट्य कला के विभिन्न रूप हैं, जो निरंतर भारतीय जनमानस के आकर्षण का कारण बने रहे।
लोकनाटक की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वह अपने लिए किसी सुव्यवस्थित मंच की माँग नहीं करता। वह आरंभ से ही मुक्त आकाश के नीचे अपने पाँव जमाता आया है। यह तो अपनी आवश्यकता के लिए अवसर के अनुसार अस्थाई मंच निर्मित करता है और उन अनिवार्यताओं से अपने-आपको बचा लेता है, जो स्थाई मंच के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। यह जननाटक पर्वों, धार्मिक उत्सवों एवं अनुष्ठानों के अवसरों पर खेले जाते रहे हैं और इनकी परंपरा बहुत पुरानी है।
आगे चलकर हमें हिंदी-नाटक का व्यवस्थित रूप दिखाई देता है। इसे हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारतेंदुयुग के नाम से परिभाषित कर सकते हैं। यद्यपि भारतेंदुयुग से पूर्व भी हिंदी-नाटक की मंचीय परंपरा विद्यमान है, भारतेंदु-पूर्व हिंदी-नाटकों की सूची में रस शैली के नाटक, संस्कृत प्रभाव वाले नाटक तथा अँग्रेज़ी नाटक के अनुवाद ही प्रमुख रूप से हमारे सामने आते हैं, लेकिन भारतेंदुयुग में इन्हें परिस्थितियों के अनुसार मोड़ा एवं विकसित किया गया। भारतेंदु ने सर्वप्रथम यह अनुभव किया कि भारतीय जनता को केवल संस्कृत परिपाटी पर आधारित नाटकों से संतुष्ट रखना समय के अनुकूल नहीं है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि पारसी रंगमंच भी भारतीय जनमानस की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा।
तब उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर नाटकों के लेखन तथा मंचन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतेंदु के उदय से हिंदी-नाट्य-कला को एक नई दिशा मिली। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि भारतेंदु न केवल आधुनिक हिंदी-नाटक के जन्मदाता हैं बल्कि समस्त हिंदी-साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के पुरोधा ऐतिहासिक महापुरुष हैं। उन्होंने और उनके समकालीन नाटककारों ने लीक से हटकर अपने-आपको समसामयिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के साथ जोड़ा तथा उद्देश्य को प्रमुखता देकर कलात्मक नाटकों, की रचना की। इन नाटककारों ने अपना ध्यान विशेष रूप में देश की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याओं की ओर केंद्रित किया। यह समय हिंदी-नाटक के लिए परिवर्तनशीलता का युग था।
पूरा देश उथल-पुथल से भरा हुआ था। यह वह समय था, जब एक ओर पुरातनवादी वर्ग अपनी सारी परंपराओं तथा रुढ़िवादी रीति-रिवाजों को ज्यों-का-त्यों बनाए रखने और उन्हें भारतीय संस्कृति का अपरिवर्तनीय आधार मानने की हठ कर रहा था तो दूसरा वर्ग प्राचीन परंपराओं एवं रूढ़ियों के बंधन से निकलकर पुनर्जागरण की ओर अग्रसर हो रहा था। ऐसी स्थिति में भारतेंदु हरिशचंद्र की दृष्टि नाट्यकला की ओर गई। क्योंकि यह कला अपनी प्राचीन परंपरा के कारण हास-परिहास अथवा मनोरंजन के दायरे से आगे नहीं निकल पा रही थी। इस नाट्य-परंपरा में कला और उद्देश्य दोनों का भारी अभाव था। इसके साथ ही रंगमंच की दशा भी शोचनीय थी। भारतेंदुयुग में यह गतिरोध टूटा और नाटक को उद्देश्यपूर्ण एवं संदर्भों के साथ जोड़कर एक व्यवस्थित रंगमंच दिया गया। इस युग में ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, राजनीतिक, रोमांटिक तथा राष्ट्रीयता प्रधान नाटक तो लिखे ही गए, साथ ही अच्छे और उच्चस्तरीय नाटकों का संस्कृत, बंगला तथा अँग्रेज़ी भाषाओं से अनुवाद भी किया गया।
यह घटना भी स्मरण कर लेनी चाहिए कि हिंदी-नाट्यकला का सबसे पहला रंगमंच काशी में 1868 में ‘बनारस थियेटर’ के नाम से स्थापित किया गया था। हिंदी-नाटक के विकास तथा रंगमंच की स्थापना की इसी पृष्ठभूमि में साहित्य के युगपुरुष जयशंकर प्रसाद का उदय हुआ। वे नाटक-रचयिता थे, अभिनेता नहीं थे। उन्होंने ऐतिहासिक विषयों से जुड़े सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले तथा भारतीय गौरव को दर्शाने वाले उच्चस्तरीय नाटक लिखे। हिंदी-नाटक को भारतेंदु ने जहाँ छोड़ा था, प्रसाद ने उसे आगे चलकर नया मोड़ दिया। प्रसाद ने हिंदी-नाटकों में ऐसे विषय भी जोड़े, जो उनसे पहले अमान्य अथवा अशोभनीय समझे जाते थे। उदाहरण के लिए हमें इन नाटकों में मंच पर ही युद्ध मृत्यु, हत्या, आत्महत्या, अपहरण, आदि-आदि के दृश्य भी दिखाई देते हैं। स्पष्ट है कि यह शैली पाश्चात्य परंपरा के प्रभाव से हिंदी-नाटकों में आई और इससे नाट्य-कला का क्षेत्र और विकसित हुआ।
यह सर्वविदित है कि भारतेंदु हरिशचंद्र के बाद का समय हिंदी-नाट्यकला के लिए विकास का उपयुक्त समय था। इस युग में गोविंदवल्लभ पंत, उग्र, सेठ गोविंददास हरिकृष्ण प्रेमी, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री तथा उदयशंकर भट्ट ने अच्छे मंचीय नाटक लिखे। इस युग में मौलिक नाटक भी लिखे गए। पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय व समस्या-प्रधान नाटक भी। इस युग में अच्छे नाटकों का विभिन्न भाषाओं से अनुवाद भी हुआ। लेकिन यह भी सही है कि जिस युग को हम ‘प्रसाद-युग’ का नाम देते हैं, वह रंगमंचीय दृष्टि से बहुत कम विकसित हुआ। प्रसाद-युग में या उसके उपरांत नाट्यकला के जिन रूपों का उदय हुआ, उनमें एकांकी की विधा अपना विशेष महत्त्व रखती है। यह एक नवीन तथा स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित भी हुई लोकप्रिय भी। एकांकी के साथ वे सारे विषय और समस्याएँ भी जुड़ गईं, जो अब तक नाट्यकला से दूर थीं।
एकांकी की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यह भी था कि इसमें समस्त आडंबरों को त्यागते हुए सामान्य जनजीवन और उससे जुड़ी समस्याओं को प्रस्तुत किया जाने लगा था। इन दैनिक समस्याओं में दर्शक अपने-आपको व्यक्तिगत रूप में सम्मिलित पाता था, जबकि पुराने राजा-महाराजाओं अथवा दैवीय घटनाओं पर रचित नाटकों से सामान्यजन की कोई संबद्धता नहीं होती थी। हिंदी में एकांकी नाटकों की रचना एवं प्रस्तुति यों तो भारतेंदु एवं द्विवेदी-युग में भी होती रही, किंतु उस समय ऐसा कोई लेखक या नाटककार उभरकर सामने नहीं आया, जो एकांकी रचना को नवीन शिल्प एवं कथा मापदंडों से जोड़ता। बाद में एकांकी को नया रूप, नई, तकनीक तथा प्रस्तुतिकरण का नया रंग-ढंग मिला।
देश की स्वतंत्रता के उपरांत हिंदी-एकांकी के विकास को और अधिक अनुकूल वातावरण मिला। उसके परिपक्व होने की संभावनाएँ और अधिक उज्ज्वल हुईं। इस प्रकार एकांकी एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित हो गया।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book