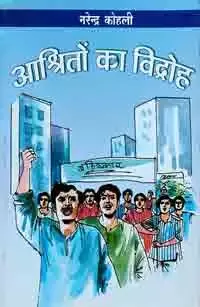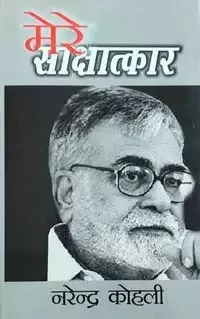|
सामाजिक >> आश्रितों का विद्रोह आश्रितों का विद्रोहनरेन्द्र कोहली
|
199 पाठक हैं |
||||||
नरेन्द्र कोहली हिंदी के जाने माने रचनाकार हैं। प्रस्तुत उपन्यास के विषयों को उन्होंने आस-पड़ोस से उठाया है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
नरेन्द्र कोहली हिंदी के जाने माने रचनाकार हैं। इनके लेखन का विकास
समाजिक विषयों के माध्यम से हुआ है। प्रस्तुत उपन्यास के विषयों को
उन्होंने आस-पड़ोस से उठाया है। इसलिए ये आपको अपने से पुनः परिचित कराता
दिखाई देगा। इनकी लेखनी की मार सहलाती है तो सालती भी है, कटाक्ष करती है
और रह-रहकर चुभन भी पैदा करती है। प्रस्तुत रचना में लेखक ने अत्यन्त सहज
भाव से समाज की विसंगतियों को उजागर किया है। इतना सहज भाव और ऐसी भेदक
दृष्टि कदाचित ही देखने को मिलती है।
प्रतीकात्मकता, विधायकता, तटस्थता, समग्र प्रभाव, समसामयिकता, समस्यात्मकता और संयम उनके व्यंग्य विधान में प्रभावी तत्व के रूप में विद्यमान दृष्टिगोचर होते हैं। लेखक के पास विराट दृष्टि, अनुभवों का खजाना है और एक सशक्त कलम है। इन तीनों के मिश्रण से उपजा है यह उपन्यास!
प्रतीकात्मकता, विधायकता, तटस्थता, समग्र प्रभाव, समसामयिकता, समस्यात्मकता और संयम उनके व्यंग्य विधान में प्रभावी तत्व के रूप में विद्यमान दृष्टिगोचर होते हैं। लेखक के पास विराट दृष्टि, अनुभवों का खजाना है और एक सशक्त कलम है। इन तीनों के मिश्रण से उपजा है यह उपन्यास!
प्रत्येक शासन-व्यवस्था में शासन की आलोचना होती है। इस आलोचना का सामना
करने का एक विज्ञान है, (उस विज्ञान का नामकरण अभी नहीं किया गया है)। उस
विज्ञान के अनुसार आलोचना को समाप्त करने की तीन प्रणालियां हैं-पहली
प्रणाली है कि जिस कार्य संस्था, पद्धति अथवा व्यक्ति की आलोचना हो, उसे
बन्द कर दिया जाये; दूसरी प्रणाली है कि पुलिस-शक्ति में वृद्धि की जाये
तथा सिपाहियों को पहले से लम्बी एवं अधिक मजबूत लाठियां दे दी जायें;
तीसरी प्रणाली है कि एक कमेटी बैठा दी जाये और उसकी रिपोर्ट पर विचार करने
के लिए एक सब-कमेटी का निर्माण कर दिया जाये। ऐसी अवस्था में प्रशासक को
कुछ नहीं करना पड़ता है। वह कमेटी की रिपोर्ट सब-कमेटी को और सब-कमेटी की
रिपोर्ट कमेटी को भेजता रहता है; तथा आलोचना की जमना जी के किनारे एक
सुन्दर समाधि बनवा देता है।
इसी पुस्तक से
आश्रितों का विद्रोह
राजधानी के एक बस-स्टाप पर बहुत भीड़ थी। प्रतीक्षा में खड़े रहनेवाले
यात्रियों के लिए दिल्ली परिवहन के योग्य अधिकारियों ने लकड़ी का एक शेड
बनवा रखा था। अपनी संस्कृति के समान ही, इस लकड़ी के शेड के बनवाये जाने
के कारण के विषय में भी लोग एकमत नहीं हैं। एक स्वीकृत मत तो यह है कि यह
शेड इसलिए बनवाया गया है कि बस की प्रतीक्षा के लिए अभिशप्त लोग, पंक्ति
में खड़े रहकर सर्दियों में धूप तथा गर्मियों में खुली हवा से वंचित
रहें।
एक अन्य विचार इसका सम्बन्ध एक पुरानी घटना से जोड़ता है। पहले जब यहां
यह
शेड नहीं था तो सर्दियों में ठण्ड खा, गर्मियों में धूप से पीड़ित हो तथा
बरसातों में भीगकर लोग बड़े उदार मन से बीमार पड़ जाया करते थे। उन लोगों
के कारण पास के अप्रतिष्ठित डॉक्टर की प्रैक्टिस खूब चल निकली थी। एक दिन
दिल्ली परिवहन के एक अधिकारी का उस डॉक्टर के साथ किसी बात पर झगड़ा हो
गया। तब उस अधिकारी द्वारा डॉक्टर का काम ठप्प करने के लिए यह शेड बनवा
दिया गया था। अपने यहां हानि पहुंचाने की दक्षता संसार-भर में अद्वितीय
है। कहते हैं कि डॉक्टर ने लोगों के बीमार पड़ने के मौलिक अधिकार के हनन
के इस प्रयत्न के विरुद्ध मुकदमा भी किया था। पर बेचारा हार गया क्योंकि
मुकदमा अस्पताल में नहीं, कचहरी में लड़ा जाता है और कचहरी में डॉक्टर का
नहीं वकील का राज होता है। एक तीसरा प्रचलित मत यह है कि यह शेड दिल्ली
परिवहन के उस अधिकारी ने बनवायी थी, जो रिटायर्ड सैनिक अफसर था। वैसे,
शेड
के आकार को देखते हुए यह बात अधिक न्याय संगत लगती है, शेड इतना कम चौड़ा
है कि लोग वहां ‘सिंगल फाइल’ में ही खड़े हो सकते
हैं। न दो लोग एक-साथ खड़े हो सकेंगे, न अनुशासन भंग होने की संभावना
होगी।
सुबह सबसे पहले एक व्यक्ति यहां आया था। और निश्चित रूप से वह बस में चढ़ने के संकल्प के साथ ही यहां आया था- यह कोई ताज महल तो है नहीं कि लोग इसे देखने के लिए आया करें। यद्यपि हमारे अधिकारी यही चाहते हैं कि लोग बस-स्टाप को एक दर्शनीय स्थान ही मानें। पर जनता को एक बुरी आदत है कि वह अधिकारियों की इच्छाओं का आदर नहीं करती और न उन्हें सहयोग देती है। इस संघर्ष का परिणाम यह हुआ है कि दिल्ली में बस स्टाप न तो बस में चढ़ने का स्थान बन पाये हैं, न दर्शनीय वस्तु ही।
वह पहला व्यक्ति भले नागरिकों के समान आकर शेड में ही खड़ा हुआ था, और शेड के भी उस विशेष स्थल पर, जो शेड से बाहर निकलने का मार्ग माना जाता है और दिल्ली परिवहन के धार्मिक नियमों के अनुसार जहां बस को रुककर, शेड को दण्डवत करना ही चाहिए। यह दूसरी बात है कि बसें अब नास्तिक हो गयीं हैं और दण्डवत करना तो दूर, वे उनके सामने से इस फर्राटे से निकल जाती हैं, जैसे मन्दिर के सामने से कोई मुसलमान और मस्जिद के सामने से कोई हिन्दू सिर ताने अपना विद्रोह जताने के लिए अकड़कर गुजर जाता है।
पहले आनेवाले उस भले नागरिक ने अपने भोले मन में यह सोच लिया था कि जब पहली बस आकर रुकेगी तो उसमें चढ़ने में उसे कोई असुविधा न होती। जैसे प्रेमचन्द्र के होरी के मन में अपने जीवन में ही गाय प्राप्त करने की चांद-हठ थी, वैसे ही उस भोले नागरिक के मन में समय पर दफ्तर पहुंच जाने की असम्भव साध थी। कुछ लोग इस असम्भव साध को क्रान्तिकारी विचार भी मानते हैं। देर से दफ्तर पहुंचने की अपनी पवित्र परम्परा को तोड़कर समय से दफ्तर पहुंचने का विचार अपने देश में उतना ही क्रान्तिकारी है जितना विदेशों की धमकियां सुनना बन्द कर अपने प्रतिरक्षा मंत्री का विदेशों को धमकियां देना। (हे प्रभु ! हमें क्षमा कर, हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। यदि हम भी धमकियां देनी आरम्भ कर देंगे तो धमकियां सुननेवाला कौन रह जायेगा। फिर दुनियावाले भारतीय किसे कहेंगे। हे प्रभु ! दुनिया को श्रोताओं के इस अकाल से उबार। नहीं तो धमकियों के साहित्य से भयंकर गतिरोध आ जायेगा।)
पर तभी वह दूसरा व्यक्ति आ गया। पहले व्यक्ति को अपनी इच्छा पूरी होने में कुछ खतरा दीखने लगा। दूसरा व्यक्ति भी उसी देश का रहने वाला था, जहां क्यू-पद्धति जहालत और दुर्बलता का प्रतीक मानी जाती है। हमारे राष्ट्रीय कवि ने कहा है न, ‘सिंहन्ह के लंहड़े नहीं हंसन्ह की नहीं पांति।’ तो अपने यहां एक-आध ही सिंह होता है जो दहाड़-वहाड़कर सो जाता है-शेष जनता हंस है, इसलिए पंक्ति में खड़ी नहीं होती। इसी कवि के दुष्प्रभाव से आज तक इस में ‘क्यू-पद्धति’ विकसित नहीं हो पायी है। मेरा सुझाव यह है कि जहां कहीं अधिकारी लोग लिखकर लगायें। ‘कृपया पंक्ति में खड़े हों,’ वहां कोष्टकों में यह भी लिख दिया जाना चाहिए,‘ आप मनुष्य हैं, हंस नहीं; अतः पंक्ति में खड़े होना आपके लिए कदापि लज्जाजनक बात नहीं है।’
तो पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के कान में डरते-डरते बड़ी शालीनता से फुसफुसाकर ‘‘भाई साहब ! लाइन यहां से शुरू होती है।’’ वैसे ही कहा, जैसे कनॉट प्लेस में विदेशी हिप्पियों के कानों में अपने देश के भले-मानुष ‘डॉलर-एक्सचेंज’ या ‘पाऊण्ड-एक्सचेंज’ फुसफुसाते रहते हैं। दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को उसी ‘यू ब्लडी इण्डियन’ मार्का दृष्टि से देखा, जैसे वे विदेशी हिप्पी अपने देश के भद्र लोगों को देखते हैं। पर इतनी शराफत उसने अवश्य दिखायी कि वह पहले व्यक्ति के आगे खड़ा नहीं हुआ। उसका वहां खड़ा होना एक दार्शनिक समस्या थी। ब्रह्म के संबंध में आज तक जितनी जिज्ञासाएँ हुई हैं, वे सारी जिज्ञासाएं एक-साथ ही उसके खड़े होने की समस्या पर लागू हो सकती थीं। संसार का कोई भी विशिष्ट दर्शक नहीं बता सकता था कि क्या वह ‘क्यू’ में खड़ा था ? क्या वह ‘क्यू’ में पहले आदमी के आगे खड़ा था ? क्या वह पहले आदमी के पीछे खड़ा था ? क्या बस में पहले चढ़ने का अधिकार उस पहले व्यक्ति का था ? इन सारी समस्याओं का समाधान केवल ‘नेति-नेति’ शैली में दिया जा सकता था; या फिर दूसरी शैली कुछ इस प्रकार हो सकती है: वह पंक्ति में खड़ा भी था; वह पहले व्यक्ति के आगे भी खड़ा था, साथ भी और पीछे भी। उसका बस में पहले चढ़ने का अधिकार था भी, क्योंकि वह पहले व्यक्ति के आगे खड़ा था; उसका बस में पहले चढ़ने का अधिकार नहीं भी था, क्योंकि वह पहले व्यक्ति के पीछे खड़ा था। वह वहां था भी, वह वहां नहीं भी था।
उसका वहां खड़े होने का ढंग बड़ा अभिव्यक्तिवादी था, अतः बड़ा कलात्मक था (क्योंकि कला अभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम है)। उसका उस कलात्मक शैली में खड़ा होना बार-बार यह प्रकट कर रहा था, जैसे पहला व्यक्ति बाद में आकर उसके मार्ग में खड़ा हो गया हो; और उसके निकल भागने में बाधा डाल रहा हो। दो-एक बार तो जैसे उसकी इस अभिव्यक्ति को ग्रहण कर उसका हाथ पहले व्यक्ति को मार्ग से हटाने के लिए आगे भी बढ़ा था, पर फिर उसके कन्धे को छूकर रुक गया था, जैसे हमारे मन्त्रीगण शत्रुओं को उनके घर तक खदेड़ने की घोषणा कर अपनी सेना को फिर अपनी सीमा के इधर ही रोक रखते हैं।
पहला व्यक्ति जीवन के व्यावहारिक तथ्यों का कुछ अधिक जानकार निकला। वह जानता था यह संकल्प नहीं संकेत है; और जीवन में संकेतों को न समझने का अभिनय ही सबसे अधिक सुविधाजनक है, जैसे बड़े से बड़े चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्ड की उपस्थिति में संकेत न समझने का बहाना कर लाल बत्ती के सामने से भैंसें सड़क पार कर जाती हैं। उन्हें कोई नहीं रोकता। कोई रोकेगा भी तो वे ‘बे-एं-एं-एं’ कहती हुई सिर झुकाकर आगे बढ़ जायेंगी। तो इस भैंसनीति का आश्रय ग्रहण कर पहला व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के उसे हटाने के प्रयत्नों की उपेक्षा करता रहा। दूसरे व्यक्ति ने अधिक बल नहीं दिया; और पहला व्यक्ति मनु-स्मृति के अनुसार नहीं, भैंस-स्मृति के अनुसार, पंक्ति में दूसरे व्यक्ति के आगे खड़ा रहने में सफल रहा। इसी से कहा भी है ‘सत्यमेव जयते।’ अर्थात् जो विजयी हो, वही सत्य है !
थोड़ी-सी देर में वहां तीसरा व्यक्ति आ गया, फिर चौथा, फिर पांचवां। अब लोग भीड़ की ओर खिंचने की अपनी सहज-वृत्ति के अन्तर्गत वहां आते जाते थे, और पहला व्यक्ति बार-बार उन्हें ‘‘और बादल, और बादल, और बादल आ रहे हैं’’ शैली में देख लेता था। वह पहला व्यक्ति था इसलिए ऐसे देख रहा था। वहां अकस्मात् आ खड़ा हुआ दिल्ली परिवहन का एक कण्डक्टर उन्हें इस शैली में नहीं देख रहा था। उसकी दृष्टि में कुछ फर्क था। (माइण्ड यू ! वह भैंगा नहीं था)। उसकी दृष्टि में ‘और पागल, और पागल, और पागल आ रहे हैं ?’’ का-सा भाव था।
बहुत सारे लोग आ गये थे, और भीड़ हो गयी थी। पर भीड़ ‘क्यू’ में खड़ी थी, इसलिए सब ‘भीड़ में अकेले’ ही लग रहे थे। ‘भीड़ में अकेले’ का फॉर्मूला उस व्यक्ति ने निकाला है, जो बहुत अनुशासनप्रिय था। वस्तुता वह फॉर्मूला ‘क्यू-पद्धति’ के लिए संसार की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक अभिव्यक्ति है।
थोड़ी देर में उस पंक्ति ने एक साम्प्रदायिक रूप ग्रहण कर लिया, क्योंकि उसमें ‘आफिस-गोअर’ नामक एक सम्प्रदाय-विशेष के लोगों की बहु-संख्या हो गयी थी। वे सब आयु की दृष्टि से अधेड़ थे। ‘यूनिफॉर्म’ या साम्प्रदायिक-चिह्न के नाम पर उनके सिर गंजे थे और वे लोग अपने सिर के मध्य भाग में स्थित ‘सरस तामरस गर्भ विभा’ को उतनी ही ममता से सहला रहे थे, जितनी ममता से मां अपनी पहली सन्तान के गालों को सहलाती है। अपवादस्वरूप कुछ चंचल लोग इस सिर-अंगुली खिलवाड़ से पोलो ग्राउण्ड में दौड़ते घोड़ों का दृश्य भी प्रस्तुत कर रहे थे। उसकी साम्प्रादायिक यूनिफॉर्म की कुछ और विशेषताएं भी थीं-उन सब की आंखों पर ऐनक कुछ इस अन्दाज में रखी हुई थी जैसे किसी महल की बैठक के शोभा-गवाक्ष में कोई शरारती बच्चा अपना कोई टूटा हुआ खिलौना अड़ा दे। उनकी कमीजों के कालर उधड़े हुए थे और ‘जाहि निकारों गेह तें, कस न भेद कहि देय’ शैली में उसकी पारिवारिक सूचनाएं दे रहे थे। निश्चित रूप से उनके कोई सुपुत्र विश्वविद्यालय में ‘थर्ड-इयर-इन-फार्स्ट-इयर-पद्धति’ में पिछले कई वर्षों से पढ़ रहे थे और स्वयं नयी कमीजें खरीदने पर अपनी पुरानी घिसी हुई कमीजें पिता-श्री को उपहार दे देते थे, जो उनके गले पड़ी हुई थीं। उनकी कमीजों का कोई-कोई टूटा बुआ बटन यह भी बताता था कि सुपुत्र-सुपुत्रियों के पश्चात् अब उनकी सुपत्नी भी उनके हाथ से निकल चुकी थी; और स्वयं अपने बटन टांकने में दक्ष नहीं थे। उनके हाथों में चमड़े के बड़े-बड़े बैग थे, जो सरकारी और गैर-सरकारी कागजों से उसी हाथों में चमड़े के बड़े-बड़े बैग थे, जो सरकारी और गैर-सरकारी कागजों से उसी प्रकार भरे पड़े थे, जैसे रद्दी के अखबारवाले कबाड़ी की साइकिल से लटकता हुआ बोरा ठुंसा होता है।
वे सब लोग अपने शरीर को उसी प्रकार पंक्ति में लगाते जा रहे थे जैसे वे अपनी मेज पर फाइलों को आगे-पीछे जमा करते जाते हैं। और अपनी आदत के अनुसार उस प्रेमिका के समान एक भी बस अभी तक नहीं आयी थी, जो वचन देकर भूल जाती है। दिल्ली में लोगों ने वचन-भंग का इतना अभ्यासी बना दिया है कि यहां वचन-भंग करनेवाली प्रेमिका की इस अदा की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। बाहर की प्रेमिकाओं को दिल्ली के प्रेमी बहुत सहनशील लगेंगे और दिल्ली की प्रेमिकाओं को बाहर के प्रेमी अत्यन्त कठोर। प्रेम के संसार में बसों का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करना एक ऐतिहासिक घटना है, पर कमबख्त इतिहासवालों ने इधर ध्यान ही नहीं दिया।
जब से पहला व्यक्ति आया था तब से अब तक तीन बसों के आने और आकर जाने का समय होकर बीत चुका था। चौथी का समय होनेवाला था। बस-स्टाप पर खड़ा कण्डक्टर-नुमा असिस्टेण्ट ट्रैफिक इन्स्पैक्टर बार-बार अपनी घड़ी देख रहा था और फिर बार-बार वह कागज देख रहा था, जिस पर बसों के आने का समय लिखा हुआ था।
‘‘क्यों साहब ! बस नहीं आयेगी ?’’ थोड़ी-थोड़ी देर बाद कोई जिज्ञासा हवा में उड़ते किसी आवारा मच्छर के समान उसके कानों से आ टकराती थी।
‘‘नहीं जनाब ! आयेगी कैसे नहीं।’’ वह मच्छर को झटक देता था।
‘‘अभी तक आयी तो कोई नहीं।’ घाव से उड़ायी गयी मक्खी के समान जिज्ञासा फिर आकर उसके कान पर बैठ जाती थी।
‘‘आ रही हैं साहब ! सब आ रही हैं।’’ वह मन्त्री शैली में आश्वासन देता हुआ मक्खियां उड़ाता जाता था, ‘‘तीसरी बस दस मिनट लेट है, दूसरी पच्चीस मिनट और पहली चालीस मिनट चौथी जब लेट होने लगेगी तो वह भी बता दूंगा।’’
तभी वहां एक और व्यक्ति आया। वह पहले आनेवालों से कुछ भिन्न प्रकार की चीज था। वह एक पूर्ण युवक था। उसका सिर काले पौधों से हरा-भरा था, जैसे उस खोपड़ी में खासी खाद भरी हो-उसकी आंखों पर ऐनक भी नहीं थी अर्थात् जीवन का अनुभव उसे विशेष नहीं था। उसके ठीक-ठाक कॉलर और बटन बता रहे थे कि उसने अपनी पत्नी को अभी अधिक सिर नहीं चढ़ाया था और शायद सन्तान-सुख ने उसकी नयी कमीजें अभी उससे नहीं छीनी थीं। उसके हाथ में चमड़े का बैग भी नहीं था, अर्थात् वह नयी पीढ़ी के उस वर्ग का सदस्य था, जिसने रेलवेवालों को हल्के सफर करने की सलाह मान ली थी। उसके हाथ में एक लंच-बॉक्स था, जो ‘मिनि-एज’ में मिनि-हैण्डबैग कहला सकता है। वह भी दफ्तर जा रहा था।
वह आकर पहले आदमी के पीछे बन गयी उस लम्बी-सी ‘क्यू’ में खड़ा नहीं हुआ। उसने एक बार देखा अवश्य कि पहले बहुत सारे लोग आये खड़े हैं और वे पंक्तिवद्ध होकर अनुशासित रूप में खड़े हैं। पर उसके कदम पंक्ति की ओर बढ़े ही नहीं-किसी युवक के कदम पुरानी पीढ़ी की ओर नहीं बढ़ते, उसी के कैसे बढ़ जाते ? पर भीतर-ही-भीतर उसका मन पीढ़ियों के संघर्ष से ऊपर उठा हुआ यह सोच रहा था कि यदि पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया, तो उस की बारी आते-आते दफ्तर में लंच-टाइम हो जायेगा। वहां उसका युवा-पीढ़ी से सम्बन्ध होने का लाइसेंस भी समय की गति को नहीं रोक पायेगा। तो वह क्या करे ? उसकी आंखों में क्षण-भर के लिए द्वन्द्व का भाव झलका और फिर उसने अपनी आयडियालॉजी बदल ली। उसकी आंखों से पंक्तिबद्ध लोगों के लिए वैसे ही घृणा भर आयी, जैसे भेड़ियों की आंखों में भेड़ों के लिए भर आती है। उसने अंग्रेजी दृष्टि से उन काले भारतियों को देखा, होंठ टेढ़े कर जरा-सा नाराज पीढ़ी की मुसकान मुसकराया; और फिर आकर शेड के मार्ग में फंसे उस पहले व्यक्ति के बगल में खड़ा हो गया।
पहले व्यक्ति का हाथ युवक के कन्धे की ओर इस प्रकार बढ़ा, जैसे जाला उतारने वाला बांस छत की नुक्कड़ों की ओर बढ़ता है, ‘‘भाई साहब ! जरा लाइन में आ जाइये।’’
युवक ने पहले व्यक्ति को पुलिस शैली में भरपेट घूरा और डकार लेने के स्थान पर उसका हाथ अपने कन्धे पर से इस प्रकार झटक दिया, जैसे वह पहले का हाथ न हो, सचमुच मकड़ा हो।
‘‘तुमने मेरी धोबी-धुली कमीज को अपने गन्दे हाथ क्यों लगाये ?’’
पहला व्यक्ति सहम गया। उसने बारी-बारी, युवक के चेहरे उसकी कमीज के छुए गये स्थान तथा अपने हाथ को देखा। बैंक-एकाऊण्ट में संचित होती चली आती पूंजी के समान, अपने जबड़ों के बीच जमा हो आयी थूक को गटक कर वह फंसी-सी आवाज में बोला, ‘‘मैंने तो केवल इतना ही कहा है कि आप लाइन में आ जाइये।’’
‘‘मुंह से कहना काफी नहीं है क्या ?’’ युवक ने नयी पीढ़ी के आक्रोश का मानवीकृ़त रूप प्रस्तुत किया, ‘‘मुझे बहरा समझ रखा है क्या। मेरी कमीज को छूने की क्या आवश्यकता थी ? मालूम है, धोबी एक कपड़े की धुलाई आजकल पच्चीस पैसे नकद लेता है।’’
‘‘माफ कीजियेगा, गलती हो गयी।’’ पहला आदमी पीछे हट गया।
युवक बड़ी देर तक आमंत्रण भरी आंखों से घूरता रहा, पर जब पहला व्यक्ति कुछ नहीं बोला और झगड़ा किसी भी प्रकार आगे नहीं बढ़ सका, तो वह एकदम निराश हो गया। उसके मन में पहले व्यक्ति की नपुंसकता के प्रति घृणा भर आयी। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर फिरा लिया और अपने क्रोध को शान्त करने के लिए, अपने होंठों को गोलाकर बनाकर सीटी बजाने लगा।
पंक्ति में पीछे खड़े लोगों में कहीं जैसे मधुमक्खी का छत्ता छेड़ दिया गया। एक तेज भनभनाहट फैल गयी।
‘‘देखिए साहब ! धक्केशाही है साफ-साफ।’’
‘‘और क्या साहब ! शराफत का तो जमाना ही नहीं रह गया।’’
‘‘अजी छोड़िए भी। किसका नाम ले रहे हैं। शराफत तो अब म्यूजियम में रखने की चीज हो गयी है। पहले म्यूजियम में जाते थे तो बहादुरशाह की शेरवानी और जीनतमहल का लहंगा ही देखते थे। अब वहां एक नयी चीज रखी गयी है लाकर। कहते हैं पुराने वक्तों की यादगार है कोई। उसका नाम शराफत है। पहले जिनके पास होती थी उन्हें शरीफ कहते थे। अब वह चीज मैनुफैक्चर नहीं होती। अगर किसी के पास पुराना स्टॉक पड़ा भी हो तो वह प्रकट नहीं होने देता। क्योंकि अब उसे लल्लूपन समझा जाता है।’’
भनभनाहट बढ़ती गयी। सब लोग कुछ-न-कुछ कह रहे थे, जैसे कोई सेमिनार हो रहा हो। पर कोई किसी से सम्बोधित नहीं था, इसलिए कोई किसी की सुन भी नहीं रहा था। युवक सब कुछ सुन रहा था पर उससे क्या। उससे प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहा जा रहा था, इसलिए वह सुन नहीं रहा था, उसे सुनाई पड़ रहा था। यह ओवर हियरिंग थी, जो बहुत विश्वसनीय नहीं थी। जो लोग बोल रहे थे, वे बोल कम रहे थे, मन का गुबार अधिक निकाल रहे थे। शिकायतें तो वे अपने घर से लेकर आये थे, युवक तो एक निमित्त मात्र था जैसे स्थायी भाव तो वासना के रूप में सहृदय के मन में पहले से ही होता है, साहित्य तो उसे रसानुभूति में बदलने का निमित्त मात्र है। उसने सोच रखा था, जब कोई उससे सीधे बात करेगा, तब वह उससे निबट लेगा। पर उससे किसी ने कुछ नहीं कहा, और उसे किसी से निबटने का कष्ट नहीं उठाना पड़ा।
थोड़ी देर के बाद मधुमक्खियां फिर से छत्ते पर आ बैठी थीं। भनभनाहट थम गयी थी। सब कुछ पूर्ववत् हो गया था। लोग अपनी आदत के अनुसार भूल गए थे कि पंक्ति के सब से पहले व्यक्ति और उस युवक में कोई झगड़ा भी हुआ था और सारी पंक्ति भुनभुना कर रह गयी थी किसी ने युवक को काटने का साहस नहीं किया था। यदि किसी के मस्तिष्क में पुरानी याद छिपकली के समान मुंह दिखाती भी तो युवक का चेहरा देखते ही छिपकली कहीं भाग जाती थी। अब वह युवक अकेला भी नहीं था। पूरी युवा पीढ़ी इकट्ठी हो गयी थी। उन सब के कपड़े पहले युवक के समान तंग और भड़कीले रंगोंवाले थे। सब की मूंछे ऐंठी हुई थीं। कलाइयों में लोहे के मोटे-मोटे कड़े थे, जो कुछ और मोटे होते तो हथकड़ियां लगते। उन सब के हाथों में लंच-बाक्स थे। वे लोग चीख-चीख कर बातें कर रहे थे, जैसे बस-स्टाप पर न खड़े हों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली में खड़े हों। वे लोग बेबात की बात पर जोर-जोर से कहकहे लगा रहे थे, अर्थात् लाइफ इन्जॉय कर रहे थे। उनकी दृष्टि में फेफड़े थकाना और लाइफ इन्जॉय करना एक ही बात थी।
पंक्ति वाले लोगों ने कछुओं के समान अपने दफ्तरों, अफसरों, फाइलों, केसों, बीवियों, बच्चों और बढ़ती हुई मंहगाई के खोल के नीचे अपना सिर छुपा लिया था। उनके लिए बाहर की दुनिया नहीं थी। वह युवक नहीं था। अतः वह झगड़ा भी नहीं हुआ था।
और वह वचन-भंजक प्रेमिका, बस, अभी तक नहीं आयी थी। फिर जैसे सूर्य कुछ और ऊपर चढ़ आया। छोटे-मोटे पक्षी भी जाग गये। वे पेड़ों पर, पेड़ों के नीचे तालाब के किनारे, खेतों में, सब जगह फैल गये और कलरव करने लगे। अर्थात् कॉलेज के लड़के-लड़कियां भी बस स्टाप पर आ गये। यह नयी नहीं, अति नवीन पीढ़ी थी, इसलिए वे न तो पंक्ति में खड़े हुए, न उस झगड़नेवाले युवक के समान पंक्ति के समानान्तर जाकर खड़े हुए। वे लोग बस स्टाप पर दूर दूर तक फैल गये थे, जैसे किसी समय महात्मा बुद्ध के उपदेश लेकर संसार में बौद्ध भिक्षु फैल गये थे। उन्हें देखकर यह नहीं लगता था कि उन्हें कॉलेज जाने की कोई जल्दी है। वे जैसे सैर करने निकले थे, जितनी हो जाये, उसी से संतुष्ट हो जाते। उन्हें बातों की भूख थी। उनके जबड़े उसी गति से चल रहे थे, जैसे भूखी भैंस के जबड़े चारा निगलते समय चलते हैं। कॉलेज का क्या था, कॉलेज अपनी जगह खड़ा था, वह कहीं भागा नहीं जा रहा था। प्राध्यापक वहां आये होंगे, वे प्रतीक्षा कर लेंगे-उन्हें वेतन इसी बात का मिलता है। कोर्स उनके बाप को खत्म कराना पड़ेगा-नहीं खत्म होगा तो घटाना पड़ेगा। पर समय बीत गया और बातें नहीं हुई, तो बातें अधूरी रह जायेंगी। बातें, बातें, बातें....
वे लोग पंक्ति के पास खड़े ही नहीं हुए, इसलिए उनका किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ। पर उनके अवतार से बस-स्टाप का वातावरण अछूता कैसे रह सकता था। संसार में कोई महान् घटना घटती है तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर सुनायी पड़ती है। पंक्ति में खड़े कछुओं ने अपनी लम्बी गर्दन खोल से निकाली, उन्हें देखा और गर्दन वापस खोल में खींच लीं, पर इस बार खोल का रंग बदल चुका था। उस नये खोल के नीचे कॉलेजों में शिष्टता की जो हत्या हो गयी थी, उस पर शोक-सभा हो रही थी। वहां ऐसा लग रहा था, जैसे लड़के का कॉलेज में भरती होना वैसा ही था, जैसे लड़के का चम्बल के बीहड़ों में जाकर डाकुओं के दल में मिल जाना। उन सारे खोलों के नीचे होनेवाली सभाएं कुछ निष्कर्षों पर सहमत हो गयी थीं-कॉलेज में आजकल पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही थी। आज के ग्रेजुएट से तो अच्छी अंग्रेजी उनके समय का चौथी पास लिख लेता था। आजकल के तो एम.ए. पास भी अंग्रेजी में ठीक से एप्लिकेशन ड्राफ्ट नहीं कर पाते थे (निश्चित रूप से कलियुग आ गया था)। अब तो जमाना ही बदल गया था। लड़के निर्लज्ज हो गये थे और लड़कियां उनकी भी अम्मांजान थीं। पंक्ति में खड़े हुए एक कछुए ने तो अभी कल ही एक लड़की को सिगरेट पीते देखा था। भगवान का अवतार तो अब होने ही वाला था, क्योंकि धरती पर पाप बहुत बढ़ गया था।
और तभी दूर से, पहले साहित्य में जैसे वसन्त आया करता था, वैसे ही बस जैसी कोई सुहावनी चीज आती दिखाई दी। लोगों ने एड़ियां उठा-उठाकर, पंजों के बल खड़े होकर, आंखों के ऊपर हथेली से छाया कर, उसी परम्परागत मुद्रा में उधर देखा, जैसे भारतीय किसान आकाश पर बादलों को ढूंढ़ता है, या सूरदास और नन्ददास की गोपियां मथुरा से आनेवाले मार्ग पर कृष्ण को देखा करती थीं। हजारों वर्षों से आज तक इस देश की मुद्रा नहीं बदली, वस्तु चाहे कितनी बदल गयी हो। वैसे बस हमारे जीवन में आज उतनी ही महत्त्वपूर्ण चीज हो गयी है, जितने महत्त्वपूर्ण गोपियों के लिए कृष्ण थे, या भारतीय किसान के जीवन में बादल हैं। इससे सहज ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो चीज हमारे जीवन में अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है, वह अवश्य ही मथुरा चली जाती है अर्थात् बाजार से गायब हो जाती है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि किसी भी चीज को अपने जीवन में इतनी अधिक महत्त्वपूर्ण मत बनने दो।
‘‘पूरे सवा घण्टे बाद बस आयी है।’’ पहले व्यक्ति ने प्रेमिका से शिकायत करने की शैली में कहा।
‘‘देखिए ए.टी.आई. साहब !’’ पंक्ति के एक अन्य कछुए ने खोल में से सिर निकाला, ‘‘अब लाइन से बस में चढ़ाइएगा। यह न हो कि हम खड़े के खड़े रह जायें और बाराती लोग बस में चढ़ जायें।’’
बस रुकी तो पंक्ति में खड़े लोगों और पंक्ति के माथे पर खड़े ए.टी.आई. की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। इस समय सामने बस खड़ी थी। बस से अधिक महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। बस रुकी कि जैसे चुम्बक ने मिट्टी, रेत, चीनी और लोहे के कणों के ढेर में से लोहे के कणों को खींच लिया और शेष चीजें वहीं की वहीं पड़ी रह गयीं। लोग बस से वैसे ही चिपक गये थे, जैसे लोहे के कण चुम्बक से चिपकते हैं; और लोहे के कण पंक्ति के बाहर-ही-बाहर थे। पंक्ति में खड़े कछुए तो रेत के कण ही प्रमाणित हुए।
सुबह सबसे पहले एक व्यक्ति यहां आया था। और निश्चित रूप से वह बस में चढ़ने के संकल्प के साथ ही यहां आया था- यह कोई ताज महल तो है नहीं कि लोग इसे देखने के लिए आया करें। यद्यपि हमारे अधिकारी यही चाहते हैं कि लोग बस-स्टाप को एक दर्शनीय स्थान ही मानें। पर जनता को एक बुरी आदत है कि वह अधिकारियों की इच्छाओं का आदर नहीं करती और न उन्हें सहयोग देती है। इस संघर्ष का परिणाम यह हुआ है कि दिल्ली में बस स्टाप न तो बस में चढ़ने का स्थान बन पाये हैं, न दर्शनीय वस्तु ही।
वह पहला व्यक्ति भले नागरिकों के समान आकर शेड में ही खड़ा हुआ था, और शेड के भी उस विशेष स्थल पर, जो शेड से बाहर निकलने का मार्ग माना जाता है और दिल्ली परिवहन के धार्मिक नियमों के अनुसार जहां बस को रुककर, शेड को दण्डवत करना ही चाहिए। यह दूसरी बात है कि बसें अब नास्तिक हो गयीं हैं और दण्डवत करना तो दूर, वे उनके सामने से इस फर्राटे से निकल जाती हैं, जैसे मन्दिर के सामने से कोई मुसलमान और मस्जिद के सामने से कोई हिन्दू सिर ताने अपना विद्रोह जताने के लिए अकड़कर गुजर जाता है।
पहले आनेवाले उस भले नागरिक ने अपने भोले मन में यह सोच लिया था कि जब पहली बस आकर रुकेगी तो उसमें चढ़ने में उसे कोई असुविधा न होती। जैसे प्रेमचन्द्र के होरी के मन में अपने जीवन में ही गाय प्राप्त करने की चांद-हठ थी, वैसे ही उस भोले नागरिक के मन में समय पर दफ्तर पहुंच जाने की असम्भव साध थी। कुछ लोग इस असम्भव साध को क्रान्तिकारी विचार भी मानते हैं। देर से दफ्तर पहुंचने की अपनी पवित्र परम्परा को तोड़कर समय से दफ्तर पहुंचने का विचार अपने देश में उतना ही क्रान्तिकारी है जितना विदेशों की धमकियां सुनना बन्द कर अपने प्रतिरक्षा मंत्री का विदेशों को धमकियां देना। (हे प्रभु ! हमें क्षमा कर, हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। यदि हम भी धमकियां देनी आरम्भ कर देंगे तो धमकियां सुननेवाला कौन रह जायेगा। फिर दुनियावाले भारतीय किसे कहेंगे। हे प्रभु ! दुनिया को श्रोताओं के इस अकाल से उबार। नहीं तो धमकियों के साहित्य से भयंकर गतिरोध आ जायेगा।)
पर तभी वह दूसरा व्यक्ति आ गया। पहले व्यक्ति को अपनी इच्छा पूरी होने में कुछ खतरा दीखने लगा। दूसरा व्यक्ति भी उसी देश का रहने वाला था, जहां क्यू-पद्धति जहालत और दुर्बलता का प्रतीक मानी जाती है। हमारे राष्ट्रीय कवि ने कहा है न, ‘सिंहन्ह के लंहड़े नहीं हंसन्ह की नहीं पांति।’ तो अपने यहां एक-आध ही सिंह होता है जो दहाड़-वहाड़कर सो जाता है-शेष जनता हंस है, इसलिए पंक्ति में खड़ी नहीं होती। इसी कवि के दुष्प्रभाव से आज तक इस में ‘क्यू-पद्धति’ विकसित नहीं हो पायी है। मेरा सुझाव यह है कि जहां कहीं अधिकारी लोग लिखकर लगायें। ‘कृपया पंक्ति में खड़े हों,’ वहां कोष्टकों में यह भी लिख दिया जाना चाहिए,‘ आप मनुष्य हैं, हंस नहीं; अतः पंक्ति में खड़े होना आपके लिए कदापि लज्जाजनक बात नहीं है।’
तो पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के कान में डरते-डरते बड़ी शालीनता से फुसफुसाकर ‘‘भाई साहब ! लाइन यहां से शुरू होती है।’’ वैसे ही कहा, जैसे कनॉट प्लेस में विदेशी हिप्पियों के कानों में अपने देश के भले-मानुष ‘डॉलर-एक्सचेंज’ या ‘पाऊण्ड-एक्सचेंज’ फुसफुसाते रहते हैं। दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को उसी ‘यू ब्लडी इण्डियन’ मार्का दृष्टि से देखा, जैसे वे विदेशी हिप्पी अपने देश के भद्र लोगों को देखते हैं। पर इतनी शराफत उसने अवश्य दिखायी कि वह पहले व्यक्ति के आगे खड़ा नहीं हुआ। उसका वहां खड़ा होना एक दार्शनिक समस्या थी। ब्रह्म के संबंध में आज तक जितनी जिज्ञासाएँ हुई हैं, वे सारी जिज्ञासाएं एक-साथ ही उसके खड़े होने की समस्या पर लागू हो सकती थीं। संसार का कोई भी विशिष्ट दर्शक नहीं बता सकता था कि क्या वह ‘क्यू’ में खड़ा था ? क्या वह ‘क्यू’ में पहले आदमी के आगे खड़ा था ? क्या वह पहले आदमी के पीछे खड़ा था ? क्या बस में पहले चढ़ने का अधिकार उस पहले व्यक्ति का था ? इन सारी समस्याओं का समाधान केवल ‘नेति-नेति’ शैली में दिया जा सकता था; या फिर दूसरी शैली कुछ इस प्रकार हो सकती है: वह पंक्ति में खड़ा भी था; वह पहले व्यक्ति के आगे भी खड़ा था, साथ भी और पीछे भी। उसका बस में पहले चढ़ने का अधिकार था भी, क्योंकि वह पहले व्यक्ति के आगे खड़ा था; उसका बस में पहले चढ़ने का अधिकार नहीं भी था, क्योंकि वह पहले व्यक्ति के पीछे खड़ा था। वह वहां था भी, वह वहां नहीं भी था।
उसका वहां खड़े होने का ढंग बड़ा अभिव्यक्तिवादी था, अतः बड़ा कलात्मक था (क्योंकि कला अभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम है)। उसका उस कलात्मक शैली में खड़ा होना बार-बार यह प्रकट कर रहा था, जैसे पहला व्यक्ति बाद में आकर उसके मार्ग में खड़ा हो गया हो; और उसके निकल भागने में बाधा डाल रहा हो। दो-एक बार तो जैसे उसकी इस अभिव्यक्ति को ग्रहण कर उसका हाथ पहले व्यक्ति को मार्ग से हटाने के लिए आगे भी बढ़ा था, पर फिर उसके कन्धे को छूकर रुक गया था, जैसे हमारे मन्त्रीगण शत्रुओं को उनके घर तक खदेड़ने की घोषणा कर अपनी सेना को फिर अपनी सीमा के इधर ही रोक रखते हैं।
पहला व्यक्ति जीवन के व्यावहारिक तथ्यों का कुछ अधिक जानकार निकला। वह जानता था यह संकल्प नहीं संकेत है; और जीवन में संकेतों को न समझने का अभिनय ही सबसे अधिक सुविधाजनक है, जैसे बड़े से बड़े चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्ड की उपस्थिति में संकेत न समझने का बहाना कर लाल बत्ती के सामने से भैंसें सड़क पार कर जाती हैं। उन्हें कोई नहीं रोकता। कोई रोकेगा भी तो वे ‘बे-एं-एं-एं’ कहती हुई सिर झुकाकर आगे बढ़ जायेंगी। तो इस भैंसनीति का आश्रय ग्रहण कर पहला व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के उसे हटाने के प्रयत्नों की उपेक्षा करता रहा। दूसरे व्यक्ति ने अधिक बल नहीं दिया; और पहला व्यक्ति मनु-स्मृति के अनुसार नहीं, भैंस-स्मृति के अनुसार, पंक्ति में दूसरे व्यक्ति के आगे खड़ा रहने में सफल रहा। इसी से कहा भी है ‘सत्यमेव जयते।’ अर्थात् जो विजयी हो, वही सत्य है !
थोड़ी-सी देर में वहां तीसरा व्यक्ति आ गया, फिर चौथा, फिर पांचवां। अब लोग भीड़ की ओर खिंचने की अपनी सहज-वृत्ति के अन्तर्गत वहां आते जाते थे, और पहला व्यक्ति बार-बार उन्हें ‘‘और बादल, और बादल, और बादल आ रहे हैं’’ शैली में देख लेता था। वह पहला व्यक्ति था इसलिए ऐसे देख रहा था। वहां अकस्मात् आ खड़ा हुआ दिल्ली परिवहन का एक कण्डक्टर उन्हें इस शैली में नहीं देख रहा था। उसकी दृष्टि में कुछ फर्क था। (माइण्ड यू ! वह भैंगा नहीं था)। उसकी दृष्टि में ‘और पागल, और पागल, और पागल आ रहे हैं ?’’ का-सा भाव था।
बहुत सारे लोग आ गये थे, और भीड़ हो गयी थी। पर भीड़ ‘क्यू’ में खड़ी थी, इसलिए सब ‘भीड़ में अकेले’ ही लग रहे थे। ‘भीड़ में अकेले’ का फॉर्मूला उस व्यक्ति ने निकाला है, जो बहुत अनुशासनप्रिय था। वस्तुता वह फॉर्मूला ‘क्यू-पद्धति’ के लिए संसार की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक अभिव्यक्ति है।
थोड़ी देर में उस पंक्ति ने एक साम्प्रदायिक रूप ग्रहण कर लिया, क्योंकि उसमें ‘आफिस-गोअर’ नामक एक सम्प्रदाय-विशेष के लोगों की बहु-संख्या हो गयी थी। वे सब आयु की दृष्टि से अधेड़ थे। ‘यूनिफॉर्म’ या साम्प्रदायिक-चिह्न के नाम पर उनके सिर गंजे थे और वे लोग अपने सिर के मध्य भाग में स्थित ‘सरस तामरस गर्भ विभा’ को उतनी ही ममता से सहला रहे थे, जितनी ममता से मां अपनी पहली सन्तान के गालों को सहलाती है। अपवादस्वरूप कुछ चंचल लोग इस सिर-अंगुली खिलवाड़ से पोलो ग्राउण्ड में दौड़ते घोड़ों का दृश्य भी प्रस्तुत कर रहे थे। उसकी साम्प्रादायिक यूनिफॉर्म की कुछ और विशेषताएं भी थीं-उन सब की आंखों पर ऐनक कुछ इस अन्दाज में रखी हुई थी जैसे किसी महल की बैठक के शोभा-गवाक्ष में कोई शरारती बच्चा अपना कोई टूटा हुआ खिलौना अड़ा दे। उनकी कमीजों के कालर उधड़े हुए थे और ‘जाहि निकारों गेह तें, कस न भेद कहि देय’ शैली में उसकी पारिवारिक सूचनाएं दे रहे थे। निश्चित रूप से उनके कोई सुपुत्र विश्वविद्यालय में ‘थर्ड-इयर-इन-फार्स्ट-इयर-पद्धति’ में पिछले कई वर्षों से पढ़ रहे थे और स्वयं नयी कमीजें खरीदने पर अपनी पुरानी घिसी हुई कमीजें पिता-श्री को उपहार दे देते थे, जो उनके गले पड़ी हुई थीं। उनकी कमीजों का कोई-कोई टूटा बुआ बटन यह भी बताता था कि सुपुत्र-सुपुत्रियों के पश्चात् अब उनकी सुपत्नी भी उनके हाथ से निकल चुकी थी; और स्वयं अपने बटन टांकने में दक्ष नहीं थे। उनके हाथों में चमड़े के बड़े-बड़े बैग थे, जो सरकारी और गैर-सरकारी कागजों से उसी हाथों में चमड़े के बड़े-बड़े बैग थे, जो सरकारी और गैर-सरकारी कागजों से उसी प्रकार भरे पड़े थे, जैसे रद्दी के अखबारवाले कबाड़ी की साइकिल से लटकता हुआ बोरा ठुंसा होता है।
वे सब लोग अपने शरीर को उसी प्रकार पंक्ति में लगाते जा रहे थे जैसे वे अपनी मेज पर फाइलों को आगे-पीछे जमा करते जाते हैं। और अपनी आदत के अनुसार उस प्रेमिका के समान एक भी बस अभी तक नहीं आयी थी, जो वचन देकर भूल जाती है। दिल्ली में लोगों ने वचन-भंग का इतना अभ्यासी बना दिया है कि यहां वचन-भंग करनेवाली प्रेमिका की इस अदा की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। बाहर की प्रेमिकाओं को दिल्ली के प्रेमी बहुत सहनशील लगेंगे और दिल्ली की प्रेमिकाओं को बाहर के प्रेमी अत्यन्त कठोर। प्रेम के संसार में बसों का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करना एक ऐतिहासिक घटना है, पर कमबख्त इतिहासवालों ने इधर ध्यान ही नहीं दिया।
जब से पहला व्यक्ति आया था तब से अब तक तीन बसों के आने और आकर जाने का समय होकर बीत चुका था। चौथी का समय होनेवाला था। बस-स्टाप पर खड़ा कण्डक्टर-नुमा असिस्टेण्ट ट्रैफिक इन्स्पैक्टर बार-बार अपनी घड़ी देख रहा था और फिर बार-बार वह कागज देख रहा था, जिस पर बसों के आने का समय लिखा हुआ था।
‘‘क्यों साहब ! बस नहीं आयेगी ?’’ थोड़ी-थोड़ी देर बाद कोई जिज्ञासा हवा में उड़ते किसी आवारा मच्छर के समान उसके कानों से आ टकराती थी।
‘‘नहीं जनाब ! आयेगी कैसे नहीं।’’ वह मच्छर को झटक देता था।
‘‘अभी तक आयी तो कोई नहीं।’ घाव से उड़ायी गयी मक्खी के समान जिज्ञासा फिर आकर उसके कान पर बैठ जाती थी।
‘‘आ रही हैं साहब ! सब आ रही हैं।’’ वह मन्त्री शैली में आश्वासन देता हुआ मक्खियां उड़ाता जाता था, ‘‘तीसरी बस दस मिनट लेट है, दूसरी पच्चीस मिनट और पहली चालीस मिनट चौथी जब लेट होने लगेगी तो वह भी बता दूंगा।’’
तभी वहां एक और व्यक्ति आया। वह पहले आनेवालों से कुछ भिन्न प्रकार की चीज था। वह एक पूर्ण युवक था। उसका सिर काले पौधों से हरा-भरा था, जैसे उस खोपड़ी में खासी खाद भरी हो-उसकी आंखों पर ऐनक भी नहीं थी अर्थात् जीवन का अनुभव उसे विशेष नहीं था। उसके ठीक-ठाक कॉलर और बटन बता रहे थे कि उसने अपनी पत्नी को अभी अधिक सिर नहीं चढ़ाया था और शायद सन्तान-सुख ने उसकी नयी कमीजें अभी उससे नहीं छीनी थीं। उसके हाथ में चमड़े का बैग भी नहीं था, अर्थात् वह नयी पीढ़ी के उस वर्ग का सदस्य था, जिसने रेलवेवालों को हल्के सफर करने की सलाह मान ली थी। उसके हाथ में एक लंच-बॉक्स था, जो ‘मिनि-एज’ में मिनि-हैण्डबैग कहला सकता है। वह भी दफ्तर जा रहा था।
वह आकर पहले आदमी के पीछे बन गयी उस लम्बी-सी ‘क्यू’ में खड़ा नहीं हुआ। उसने एक बार देखा अवश्य कि पहले बहुत सारे लोग आये खड़े हैं और वे पंक्तिवद्ध होकर अनुशासित रूप में खड़े हैं। पर उसके कदम पंक्ति की ओर बढ़े ही नहीं-किसी युवक के कदम पुरानी पीढ़ी की ओर नहीं बढ़ते, उसी के कैसे बढ़ जाते ? पर भीतर-ही-भीतर उसका मन पीढ़ियों के संघर्ष से ऊपर उठा हुआ यह सोच रहा था कि यदि पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया, तो उस की बारी आते-आते दफ्तर में लंच-टाइम हो जायेगा। वहां उसका युवा-पीढ़ी से सम्बन्ध होने का लाइसेंस भी समय की गति को नहीं रोक पायेगा। तो वह क्या करे ? उसकी आंखों में क्षण-भर के लिए द्वन्द्व का भाव झलका और फिर उसने अपनी आयडियालॉजी बदल ली। उसकी आंखों से पंक्तिबद्ध लोगों के लिए वैसे ही घृणा भर आयी, जैसे भेड़ियों की आंखों में भेड़ों के लिए भर आती है। उसने अंग्रेजी दृष्टि से उन काले भारतियों को देखा, होंठ टेढ़े कर जरा-सा नाराज पीढ़ी की मुसकान मुसकराया; और फिर आकर शेड के मार्ग में फंसे उस पहले व्यक्ति के बगल में खड़ा हो गया।
पहले व्यक्ति का हाथ युवक के कन्धे की ओर इस प्रकार बढ़ा, जैसे जाला उतारने वाला बांस छत की नुक्कड़ों की ओर बढ़ता है, ‘‘भाई साहब ! जरा लाइन में आ जाइये।’’
युवक ने पहले व्यक्ति को पुलिस शैली में भरपेट घूरा और डकार लेने के स्थान पर उसका हाथ अपने कन्धे पर से इस प्रकार झटक दिया, जैसे वह पहले का हाथ न हो, सचमुच मकड़ा हो।
‘‘तुमने मेरी धोबी-धुली कमीज को अपने गन्दे हाथ क्यों लगाये ?’’
पहला व्यक्ति सहम गया। उसने बारी-बारी, युवक के चेहरे उसकी कमीज के छुए गये स्थान तथा अपने हाथ को देखा। बैंक-एकाऊण्ट में संचित होती चली आती पूंजी के समान, अपने जबड़ों के बीच जमा हो आयी थूक को गटक कर वह फंसी-सी आवाज में बोला, ‘‘मैंने तो केवल इतना ही कहा है कि आप लाइन में आ जाइये।’’
‘‘मुंह से कहना काफी नहीं है क्या ?’’ युवक ने नयी पीढ़ी के आक्रोश का मानवीकृ़त रूप प्रस्तुत किया, ‘‘मुझे बहरा समझ रखा है क्या। मेरी कमीज को छूने की क्या आवश्यकता थी ? मालूम है, धोबी एक कपड़े की धुलाई आजकल पच्चीस पैसे नकद लेता है।’’
‘‘माफ कीजियेगा, गलती हो गयी।’’ पहला आदमी पीछे हट गया।
युवक बड़ी देर तक आमंत्रण भरी आंखों से घूरता रहा, पर जब पहला व्यक्ति कुछ नहीं बोला और झगड़ा किसी भी प्रकार आगे नहीं बढ़ सका, तो वह एकदम निराश हो गया। उसके मन में पहले व्यक्ति की नपुंसकता के प्रति घृणा भर आयी। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर फिरा लिया और अपने क्रोध को शान्त करने के लिए, अपने होंठों को गोलाकर बनाकर सीटी बजाने लगा।
पंक्ति में पीछे खड़े लोगों में कहीं जैसे मधुमक्खी का छत्ता छेड़ दिया गया। एक तेज भनभनाहट फैल गयी।
‘‘देखिए साहब ! धक्केशाही है साफ-साफ।’’
‘‘और क्या साहब ! शराफत का तो जमाना ही नहीं रह गया।’’
‘‘अजी छोड़िए भी। किसका नाम ले रहे हैं। शराफत तो अब म्यूजियम में रखने की चीज हो गयी है। पहले म्यूजियम में जाते थे तो बहादुरशाह की शेरवानी और जीनतमहल का लहंगा ही देखते थे। अब वहां एक नयी चीज रखी गयी है लाकर। कहते हैं पुराने वक्तों की यादगार है कोई। उसका नाम शराफत है। पहले जिनके पास होती थी उन्हें शरीफ कहते थे। अब वह चीज मैनुफैक्चर नहीं होती। अगर किसी के पास पुराना स्टॉक पड़ा भी हो तो वह प्रकट नहीं होने देता। क्योंकि अब उसे लल्लूपन समझा जाता है।’’
भनभनाहट बढ़ती गयी। सब लोग कुछ-न-कुछ कह रहे थे, जैसे कोई सेमिनार हो रहा हो। पर कोई किसी से सम्बोधित नहीं था, इसलिए कोई किसी की सुन भी नहीं रहा था। युवक सब कुछ सुन रहा था पर उससे क्या। उससे प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहा जा रहा था, इसलिए वह सुन नहीं रहा था, उसे सुनाई पड़ रहा था। यह ओवर हियरिंग थी, जो बहुत विश्वसनीय नहीं थी। जो लोग बोल रहे थे, वे बोल कम रहे थे, मन का गुबार अधिक निकाल रहे थे। शिकायतें तो वे अपने घर से लेकर आये थे, युवक तो एक निमित्त मात्र था जैसे स्थायी भाव तो वासना के रूप में सहृदय के मन में पहले से ही होता है, साहित्य तो उसे रसानुभूति में बदलने का निमित्त मात्र है। उसने सोच रखा था, जब कोई उससे सीधे बात करेगा, तब वह उससे निबट लेगा। पर उससे किसी ने कुछ नहीं कहा, और उसे किसी से निबटने का कष्ट नहीं उठाना पड़ा।
थोड़ी देर के बाद मधुमक्खियां फिर से छत्ते पर आ बैठी थीं। भनभनाहट थम गयी थी। सब कुछ पूर्ववत् हो गया था। लोग अपनी आदत के अनुसार भूल गए थे कि पंक्ति के सब से पहले व्यक्ति और उस युवक में कोई झगड़ा भी हुआ था और सारी पंक्ति भुनभुना कर रह गयी थी किसी ने युवक को काटने का साहस नहीं किया था। यदि किसी के मस्तिष्क में पुरानी याद छिपकली के समान मुंह दिखाती भी तो युवक का चेहरा देखते ही छिपकली कहीं भाग जाती थी। अब वह युवक अकेला भी नहीं था। पूरी युवा पीढ़ी इकट्ठी हो गयी थी। उन सब के कपड़े पहले युवक के समान तंग और भड़कीले रंगोंवाले थे। सब की मूंछे ऐंठी हुई थीं। कलाइयों में लोहे के मोटे-मोटे कड़े थे, जो कुछ और मोटे होते तो हथकड़ियां लगते। उन सब के हाथों में लंच-बाक्स थे। वे लोग चीख-चीख कर बातें कर रहे थे, जैसे बस-स्टाप पर न खड़े हों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली में खड़े हों। वे लोग बेबात की बात पर जोर-जोर से कहकहे लगा रहे थे, अर्थात् लाइफ इन्जॉय कर रहे थे। उनकी दृष्टि में फेफड़े थकाना और लाइफ इन्जॉय करना एक ही बात थी।
पंक्ति वाले लोगों ने कछुओं के समान अपने दफ्तरों, अफसरों, फाइलों, केसों, बीवियों, बच्चों और बढ़ती हुई मंहगाई के खोल के नीचे अपना सिर छुपा लिया था। उनके लिए बाहर की दुनिया नहीं थी। वह युवक नहीं था। अतः वह झगड़ा भी नहीं हुआ था।
और वह वचन-भंजक प्रेमिका, बस, अभी तक नहीं आयी थी। फिर जैसे सूर्य कुछ और ऊपर चढ़ आया। छोटे-मोटे पक्षी भी जाग गये। वे पेड़ों पर, पेड़ों के नीचे तालाब के किनारे, खेतों में, सब जगह फैल गये और कलरव करने लगे। अर्थात् कॉलेज के लड़के-लड़कियां भी बस स्टाप पर आ गये। यह नयी नहीं, अति नवीन पीढ़ी थी, इसलिए वे न तो पंक्ति में खड़े हुए, न उस झगड़नेवाले युवक के समान पंक्ति के समानान्तर जाकर खड़े हुए। वे लोग बस स्टाप पर दूर दूर तक फैल गये थे, जैसे किसी समय महात्मा बुद्ध के उपदेश लेकर संसार में बौद्ध भिक्षु फैल गये थे। उन्हें देखकर यह नहीं लगता था कि उन्हें कॉलेज जाने की कोई जल्दी है। वे जैसे सैर करने निकले थे, जितनी हो जाये, उसी से संतुष्ट हो जाते। उन्हें बातों की भूख थी। उनके जबड़े उसी गति से चल रहे थे, जैसे भूखी भैंस के जबड़े चारा निगलते समय चलते हैं। कॉलेज का क्या था, कॉलेज अपनी जगह खड़ा था, वह कहीं भागा नहीं जा रहा था। प्राध्यापक वहां आये होंगे, वे प्रतीक्षा कर लेंगे-उन्हें वेतन इसी बात का मिलता है। कोर्स उनके बाप को खत्म कराना पड़ेगा-नहीं खत्म होगा तो घटाना पड़ेगा। पर समय बीत गया और बातें नहीं हुई, तो बातें अधूरी रह जायेंगी। बातें, बातें, बातें....
वे लोग पंक्ति के पास खड़े ही नहीं हुए, इसलिए उनका किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ। पर उनके अवतार से बस-स्टाप का वातावरण अछूता कैसे रह सकता था। संसार में कोई महान् घटना घटती है तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर सुनायी पड़ती है। पंक्ति में खड़े कछुओं ने अपनी लम्बी गर्दन खोल से निकाली, उन्हें देखा और गर्दन वापस खोल में खींच लीं, पर इस बार खोल का रंग बदल चुका था। उस नये खोल के नीचे कॉलेजों में शिष्टता की जो हत्या हो गयी थी, उस पर शोक-सभा हो रही थी। वहां ऐसा लग रहा था, जैसे लड़के का कॉलेज में भरती होना वैसा ही था, जैसे लड़के का चम्बल के बीहड़ों में जाकर डाकुओं के दल में मिल जाना। उन सारे खोलों के नीचे होनेवाली सभाएं कुछ निष्कर्षों पर सहमत हो गयी थीं-कॉलेज में आजकल पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही थी। आज के ग्रेजुएट से तो अच्छी अंग्रेजी उनके समय का चौथी पास लिख लेता था। आजकल के तो एम.ए. पास भी अंग्रेजी में ठीक से एप्लिकेशन ड्राफ्ट नहीं कर पाते थे (निश्चित रूप से कलियुग आ गया था)। अब तो जमाना ही बदल गया था। लड़के निर्लज्ज हो गये थे और लड़कियां उनकी भी अम्मांजान थीं। पंक्ति में खड़े हुए एक कछुए ने तो अभी कल ही एक लड़की को सिगरेट पीते देखा था। भगवान का अवतार तो अब होने ही वाला था, क्योंकि धरती पर पाप बहुत बढ़ गया था।
और तभी दूर से, पहले साहित्य में जैसे वसन्त आया करता था, वैसे ही बस जैसी कोई सुहावनी चीज आती दिखाई दी। लोगों ने एड़ियां उठा-उठाकर, पंजों के बल खड़े होकर, आंखों के ऊपर हथेली से छाया कर, उसी परम्परागत मुद्रा में उधर देखा, जैसे भारतीय किसान आकाश पर बादलों को ढूंढ़ता है, या सूरदास और नन्ददास की गोपियां मथुरा से आनेवाले मार्ग पर कृष्ण को देखा करती थीं। हजारों वर्षों से आज तक इस देश की मुद्रा नहीं बदली, वस्तु चाहे कितनी बदल गयी हो। वैसे बस हमारे जीवन में आज उतनी ही महत्त्वपूर्ण चीज हो गयी है, जितने महत्त्वपूर्ण गोपियों के लिए कृष्ण थे, या भारतीय किसान के जीवन में बादल हैं। इससे सहज ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो चीज हमारे जीवन में अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है, वह अवश्य ही मथुरा चली जाती है अर्थात् बाजार से गायब हो जाती है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि किसी भी चीज को अपने जीवन में इतनी अधिक महत्त्वपूर्ण मत बनने दो।
‘‘पूरे सवा घण्टे बाद बस आयी है।’’ पहले व्यक्ति ने प्रेमिका से शिकायत करने की शैली में कहा।
‘‘देखिए ए.टी.आई. साहब !’’ पंक्ति के एक अन्य कछुए ने खोल में से सिर निकाला, ‘‘अब लाइन से बस में चढ़ाइएगा। यह न हो कि हम खड़े के खड़े रह जायें और बाराती लोग बस में चढ़ जायें।’’
बस रुकी तो पंक्ति में खड़े लोगों और पंक्ति के माथे पर खड़े ए.टी.आई. की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। इस समय सामने बस खड़ी थी। बस से अधिक महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। बस रुकी कि जैसे चुम्बक ने मिट्टी, रेत, चीनी और लोहे के कणों के ढेर में से लोहे के कणों को खींच लिया और शेष चीजें वहीं की वहीं पड़ी रह गयीं। लोग बस से वैसे ही चिपक गये थे, जैसे लोहे के कण चुम्बक से चिपकते हैं; और लोहे के कण पंक्ति के बाहर-ही-बाहर थे। पंक्ति में खड़े कछुए तो रेत के कण ही प्रमाणित हुए।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book