|
नारी विमर्श >> चल खुसरो घर आपने (अजिल्द) चल खुसरो घर आपने (अजिल्द)शिवानी
|
170 पाठक हैं |
||||||
अन्य सभी उपन्यासों की भाँति शिवानी का यह उपन्यास भी पाठक को मंत्र-मुग्ध कर देने में समर्थ है
...‘कैसी विचित्र पुतलियाँ लग रही थीं मालती की। जैसे दगदगाती हीरे की दो कनियाँ हों, बार-बार वह अपनी पतली जिह्वा को अपने रक्तवर्णी अधरों पर फेर रही थी, यह तो नित्य की सौम्य-शान्त स्वामिनी नहीं, जैसे भयंकर अग्निशिखा लपटें ले रही थीं...।’ यह कहानी है कुमुद की, जिसे बिगड़ैल भाई-बहनों और आर्थिक, पारिवारिक परिस्थितियों ने सुदूर बंगाल जाकर एक राजासाहब की मानसिक रूप से बीमार पत्नी की परिचर्या का दुरूह भार थमा दिया है।
मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का मनोसंसार, निम्नमध्यवर्गीय परिवार की कमासुत अनब्याही बेटी और उसकी ग्लानि से दबी जाती माँ का मनोविज्ञान, ‘शिवानी’ के पारस स्पर्श से समृद्ध होकर इस उपन्यास को एक अद्भुत नाटकीय कलेवर और पठनीयता देते हैं।
शिवानी का ‘विवर्त्त’ मानव जीवन की रहस्यमयता का एक विलक्षण पहलू प्रस्तुत करता है। चरित्र-नायिका ललिता गरीब माता-पिता की सात पुत्रियों में सबसे छोटी होने पर भी स्वतंत्र-मेधा और तेजस्विनी है और डबल एम.ए. करके हेडमिस्ट्रेस बन जाती है। वह विवाह नहीं करना चाहती और आने वाले सभी रिश्तों को ठुकरा देती है परन्तु प्रारब्ध उसके साथ ऐसा खेल खेलता है कि वह स्तब्ध रह जाती है।
अपने अन्य सभी उपन्यासों की भाँति शिवानी का यह उपन्यास भी पाठक को मंत्र-मुग्ध कर देने में समर्थ है।
मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का मनोसंसार, निम्नमध्यवर्गीय परिवार की कमासुत अनब्याही बेटी और उसकी ग्लानि से दबी जाती माँ का मनोविज्ञान, ‘शिवानी’ के पारस स्पर्श से समृद्ध होकर इस उपन्यास को एक अद्भुत नाटकीय कलेवर और पठनीयता देते हैं।
शिवानी का ‘विवर्त्त’ मानव जीवन की रहस्यमयता का एक विलक्षण पहलू प्रस्तुत करता है। चरित्र-नायिका ललिता गरीब माता-पिता की सात पुत्रियों में सबसे छोटी होने पर भी स्वतंत्र-मेधा और तेजस्विनी है और डबल एम.ए. करके हेडमिस्ट्रेस बन जाती है। वह विवाह नहीं करना चाहती और आने वाले सभी रिश्तों को ठुकरा देती है परन्तु प्रारब्ध उसके साथ ऐसा खेल खेलता है कि वह स्तब्ध रह जाती है।
अपने अन्य सभी उपन्यासों की भाँति शिवानी का यह उपन्यास भी पाठक को मंत्र-मुग्ध कर देने में समर्थ है।
चल खुसरो घर आपने
अपना सूटकेस हाथ में लटकाए ही वह उतर गई। एक क्षण को, उस बियाबान स्टेशन का
सन्नाटा, उसे सहमा गया था। यदि, कोई उसे लेने आया तब? क्या करेगी वह? एक
लुंगीधारी काला कदर्य व्यक्ति, उसे घूरे जा रहा था। अचानक, अम्मा के सरल
घबराए चेहरे की स्मृति, उसे विकल कर उठी! कितनी बार अम्मा, उसे समझा-बुझाकर
हार गई थी : 'मुझे तेरा उतनी दूर जाना, जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है कुमू :
चार दिन रुक जाती तो मैं बड़े भैया को बुला लेती, तुझे पहुँचा भी आते और देख
भी आते कि कैसे लोग हैं। और फिर, तेरी यहाँ की नौकरी कौन बुरी है? अखबारी
विज्ञापन का क्या ठिकाना? अभी कहते हैं इतनी तनख्वाह देंगे, जब न दें तो तू
अकेली उस अनजान शहर में क्या कर लेगी?'
किन्तु, कुमुद को उस शहर का एक-एक पल जैसे काट खाने को दौड़ रहा था। धर्मभीरू अम्मा का, छोटी बहन उमा का, जिसे उसने कुछ ही दिन पहले मार-मार कर बेदम कर दिया था, और छोटे उद्दण्ड भाई लालू का सान्निध्य, अब वह जैसे एक पल भी सह नहीं पा रही थी। उसने यह निश्चय बहुत सोच-विचार कर ही किया था, प्रत्येक सम्भावना को उसने रात-रात जगकर अपने विवेक की तुला से तौल कर ही इतनी दूर आने का फैसला किया था। वह कुछ दिन और लखनऊ रह जाती तो निश्चय ही मानसिक सन्तुलन खो बैठती। उमा ने क्या उसे कहीं मुँह दिखाने लायक रखा था? उसे लगने लगा था कि भाई, बहन, माँ प्रतिवेशी सब उसके दुश्मन बने-भाला लिये उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। सहसा उस बीहड़-से स्टेशन में खड़ी कुमुद का हृदय, एक अज्ञात आशंका से काँप उठा। अम्मा ने ठीक ही कहा था, ऐसे उन अनजान शहर में उसका बिना किसी से कुछ पूछे केवल एक पत्र का सूत्र पकड़ चले आना, बचपना मात्र था। वह एक बार फिर, इधर-उधर देखने लगी, तार तो उसने भेज दिया था, तब भी क्या कोई उसे लेने नहीं आया?
"मिस साहब!" वही लुंगीधारी सहसा उसकी ओर बढ़ आया-"माफ करें सरकार, आप लखनऊ से तो नहीं आईं?"
"हाँ क्यों?" कुमुद ने कुछ सहमकर ही उसे सन्दिग्ध दृष्टि से देखा।
“साहब ने हमें लेने भेजा है, खुद आ रहे थे, पर रानी साहिबा की तबीयत खराब हो गई, कहने लगे-नूरबक्श तुम्हीं चले जाओ। लाइए हुजूर, सूटकेस मुझे दीजिए।"
बड़ी सधी नम्रता से उसने, उसके हाथ से सूटकेस ले लिया और आगे-आगे चलने लगा। अपनी बड़ी-बड़ी सहमी आँखों से इधर-उधर देखती कुमुद, उसके पीछे-पीछे चली जा रही थी। एक-एक पैर, जैसे बीस-बीस सेर का हुआ जा रहा था; यदि यह कोई गुंडा हुआ तब? यदि, साहब का भेजा गया आदमी था, तो पहले दूर ही खड़ा-खड़ा, उतनी देर से उसे क्यों घूरे जा रहा था? पहले ही क्यों न लपड़ आया? इतनी देर तक, वह क्या कोई कुटिल योजना बना रहा था? उसे पहचानने में उसे इतना समय क्यों लग गया? उस छोटे से स्टेशन पर, उस ट्रेन से उतरनेवाली वही तो एकमात्र सभ्य महिला थी, जो दो-तीन बक्से-बुक्से लेकर उतरी भी थीं, बाकी सब भुच्च देहातिनें थी। खैर, बाहर चलकर देख लेगी, यदि कार आई होगी तो सन्देह का प्रश्न ही नहीं उठता था, यदि गुंडा ही होता तो कैसे जान लेता कि इस ट्रेन से वही उतरेगी?
स्टेशन का बहिरंग उसे और भी उजड़ा वीरान लगा, एक लाइन में खड़े कुछ मरियल से घोड़े-जुते इक्के, फर्श पर पसरे यात्री, बुर्काधारिणी पच्च-पच्च पान थूकती महिलाएँ, रिरियाते बच्चे। दुर्गन्ध के तीव्र भभके के बीच से, तीर सी निकल बाहर आई तो जैसे जान में जान आई।
"आइए सरकार, आप बैठे, मैं सूटकेस पीछे रख दूँ," उसने कार का द्वार खोला, रेशमी लेस लगे पर्दो में सँवरी, उस फिएट को देख, कुमुद आश्वस्त होकर बैठ गई। "क्या नाम है तुम्हारा?" कार नम्बर उसने मन-ही-मन नोट कर लिया था, चालक का नाम भी उसे जान लेना चाहिए, वह बड़ी देर से यही सोचकर भी संकोचवश नाम नहीं पूछ पा रही थी।
“जी, नूरबक्श कहते हैं खादिम को!"
"नूरबक्श, यहाँ से कितनी दूर अभी और जाना होगा?"
दिन ढल चुका था, उस उजाड़ कस्बे की वीरानी भी जैसे पुरवैया झोंके के साथ-साथ, उससे लिपटती जा रही थी। उस भयावह चेहरे के चालक के साथ, उसे अकेली जाने में, एक बार फिर एक अजीब भय की सुरसुरी उसके सर्वांग को सिहरा गई।
“यही कोई दस किलोमीटर होगी साहब की कोठी-बस ये चले और ये पहुँचे!"
"हे राम, दस किलोमीटर!" कोई अजनबी भी यदि उस पल, कुमुद से कार चलने से पूर्व, वहीं उतर लखनऊ चलने का प्रस्ताव रखता तो वह शायद, तत्काल वहीं उतर पड़ती। यह कैसी मूर्खता कर बैठी थी, वह! क्या आए दिन, अखबारों में वह ऐसी घटनाएँ नहीं पढ़ चुकी थी?
“चलें हुजूर?" सहसा उस रहस्यमय विनम्र चालक ने पूछा तो वह चौंक पड़ी-
"चलो!" और कुमुद ने निढाल होकर सीट पर पीठ साध ली। जब ओखली में सर दे ही दिया, तो मूसली से कैसा डर!
पिछले पन्द्रह दिनों के कटु अनुभवों ने उसे बुरी तरह तोड़कर रख दिया था। उद्दण्ड भाई की अबाध्यता, छोटी बहन का निर्लज्ज आचरण, निरीह अम्मा की विवशता-किसी को भी वह क्षमा नहीं कर पा रही थी। यह सब न हुआ होता तो वह शायद लखनऊ कभी न छोड़ती।
उस अन्धकारमयी निर्जन सड़क पर, तेजी से भागी जा रही कार में बैठी कुमुद की आँखें छलछला आईं। उसके बिना अम्मा कितनी असहाय हो उठेगी! कौन उसका राशन लाकर धरेगा, मकान का किराया, बिजली का बिल, पिता की पेंशन, उसका सब काम कौन करेगा! अम्मा ने दबी जबान से यह सब उससे कहा भी था-"कुमुद, मैं जानती हूँ तू हम से रूठ कर जा रही है, पर हमारा क्या होगा, यह भी तूने सोचा है? मैं जानती हूँ कि अभागों ने तेरी ही थाली में खाकर, उसी में छेद किया है, पर तू यह भी जानती है कि तू चली गई तो वे दोनों मुझे लटू-सा नचाएँगे। कोई भी अच्छा लड़का मिलता तो मैं, इस कुलबोरनी को तो विदा कर देती, पर..." फिर अम्मा, स्वयं ही अपने अज्ञानवश मुँह से निकल गई, उस अस्वाभाविक कामना के लिए खिसिया कर कहने लगी थी-"...पर मैं, क्या कभी ऐसा होने दूंगी! भले ही लाख अच्छे रिश्ते मिलें, वही होगा, जो हमारे कुल में सदा होता आया है। घर की बड़ी लड़की पहले विदा होगी, तब छोटी..."
किन्तु, कुमुद को उस शहर का एक-एक पल जैसे काट खाने को दौड़ रहा था। धर्मभीरू अम्मा का, छोटी बहन उमा का, जिसे उसने कुछ ही दिन पहले मार-मार कर बेदम कर दिया था, और छोटे उद्दण्ड भाई लालू का सान्निध्य, अब वह जैसे एक पल भी सह नहीं पा रही थी। उसने यह निश्चय बहुत सोच-विचार कर ही किया था, प्रत्येक सम्भावना को उसने रात-रात जगकर अपने विवेक की तुला से तौल कर ही इतनी दूर आने का फैसला किया था। वह कुछ दिन और लखनऊ रह जाती तो निश्चय ही मानसिक सन्तुलन खो बैठती। उमा ने क्या उसे कहीं मुँह दिखाने लायक रखा था? उसे लगने लगा था कि भाई, बहन, माँ प्रतिवेशी सब उसके दुश्मन बने-भाला लिये उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। सहसा उस बीहड़-से स्टेशन में खड़ी कुमुद का हृदय, एक अज्ञात आशंका से काँप उठा। अम्मा ने ठीक ही कहा था, ऐसे उन अनजान शहर में उसका बिना किसी से कुछ पूछे केवल एक पत्र का सूत्र पकड़ चले आना, बचपना मात्र था। वह एक बार फिर, इधर-उधर देखने लगी, तार तो उसने भेज दिया था, तब भी क्या कोई उसे लेने नहीं आया?
"मिस साहब!" वही लुंगीधारी सहसा उसकी ओर बढ़ आया-"माफ करें सरकार, आप लखनऊ से तो नहीं आईं?"
"हाँ क्यों?" कुमुद ने कुछ सहमकर ही उसे सन्दिग्ध दृष्टि से देखा।
“साहब ने हमें लेने भेजा है, खुद आ रहे थे, पर रानी साहिबा की तबीयत खराब हो गई, कहने लगे-नूरबक्श तुम्हीं चले जाओ। लाइए हुजूर, सूटकेस मुझे दीजिए।"
बड़ी सधी नम्रता से उसने, उसके हाथ से सूटकेस ले लिया और आगे-आगे चलने लगा। अपनी बड़ी-बड़ी सहमी आँखों से इधर-उधर देखती कुमुद, उसके पीछे-पीछे चली जा रही थी। एक-एक पैर, जैसे बीस-बीस सेर का हुआ जा रहा था; यदि यह कोई गुंडा हुआ तब? यदि, साहब का भेजा गया आदमी था, तो पहले दूर ही खड़ा-खड़ा, उतनी देर से उसे क्यों घूरे जा रहा था? पहले ही क्यों न लपड़ आया? इतनी देर तक, वह क्या कोई कुटिल योजना बना रहा था? उसे पहचानने में उसे इतना समय क्यों लग गया? उस छोटे से स्टेशन पर, उस ट्रेन से उतरनेवाली वही तो एकमात्र सभ्य महिला थी, जो दो-तीन बक्से-बुक्से लेकर उतरी भी थीं, बाकी सब भुच्च देहातिनें थी। खैर, बाहर चलकर देख लेगी, यदि कार आई होगी तो सन्देह का प्रश्न ही नहीं उठता था, यदि गुंडा ही होता तो कैसे जान लेता कि इस ट्रेन से वही उतरेगी?
स्टेशन का बहिरंग उसे और भी उजड़ा वीरान लगा, एक लाइन में खड़े कुछ मरियल से घोड़े-जुते इक्के, फर्श पर पसरे यात्री, बुर्काधारिणी पच्च-पच्च पान थूकती महिलाएँ, रिरियाते बच्चे। दुर्गन्ध के तीव्र भभके के बीच से, तीर सी निकल बाहर आई तो जैसे जान में जान आई।
"आइए सरकार, आप बैठे, मैं सूटकेस पीछे रख दूँ," उसने कार का द्वार खोला, रेशमी लेस लगे पर्दो में सँवरी, उस फिएट को देख, कुमुद आश्वस्त होकर बैठ गई। "क्या नाम है तुम्हारा?" कार नम्बर उसने मन-ही-मन नोट कर लिया था, चालक का नाम भी उसे जान लेना चाहिए, वह बड़ी देर से यही सोचकर भी संकोचवश नाम नहीं पूछ पा रही थी।
“जी, नूरबक्श कहते हैं खादिम को!"
"नूरबक्श, यहाँ से कितनी दूर अभी और जाना होगा?"
दिन ढल चुका था, उस उजाड़ कस्बे की वीरानी भी जैसे पुरवैया झोंके के साथ-साथ, उससे लिपटती जा रही थी। उस भयावह चेहरे के चालक के साथ, उसे अकेली जाने में, एक बार फिर एक अजीब भय की सुरसुरी उसके सर्वांग को सिहरा गई।
“यही कोई दस किलोमीटर होगी साहब की कोठी-बस ये चले और ये पहुँचे!"
"हे राम, दस किलोमीटर!" कोई अजनबी भी यदि उस पल, कुमुद से कार चलने से पूर्व, वहीं उतर लखनऊ चलने का प्रस्ताव रखता तो वह शायद, तत्काल वहीं उतर पड़ती। यह कैसी मूर्खता कर बैठी थी, वह! क्या आए दिन, अखबारों में वह ऐसी घटनाएँ नहीं पढ़ चुकी थी?
“चलें हुजूर?" सहसा उस रहस्यमय विनम्र चालक ने पूछा तो वह चौंक पड़ी-
"चलो!" और कुमुद ने निढाल होकर सीट पर पीठ साध ली। जब ओखली में सर दे ही दिया, तो मूसली से कैसा डर!
पिछले पन्द्रह दिनों के कटु अनुभवों ने उसे बुरी तरह तोड़कर रख दिया था। उद्दण्ड भाई की अबाध्यता, छोटी बहन का निर्लज्ज आचरण, निरीह अम्मा की विवशता-किसी को भी वह क्षमा नहीं कर पा रही थी। यह सब न हुआ होता तो वह शायद लखनऊ कभी न छोड़ती।
उस अन्धकारमयी निर्जन सड़क पर, तेजी से भागी जा रही कार में बैठी कुमुद की आँखें छलछला आईं। उसके बिना अम्मा कितनी असहाय हो उठेगी! कौन उसका राशन लाकर धरेगा, मकान का किराया, बिजली का बिल, पिता की पेंशन, उसका सब काम कौन करेगा! अम्मा ने दबी जबान से यह सब उससे कहा भी था-"कुमुद, मैं जानती हूँ तू हम से रूठ कर जा रही है, पर हमारा क्या होगा, यह भी तूने सोचा है? मैं जानती हूँ कि अभागों ने तेरी ही थाली में खाकर, उसी में छेद किया है, पर तू यह भी जानती है कि तू चली गई तो वे दोनों मुझे लटू-सा नचाएँगे। कोई भी अच्छा लड़का मिलता तो मैं, इस कुलबोरनी को तो विदा कर देती, पर..." फिर अम्मा, स्वयं ही अपने अज्ञानवश मुँह से निकल गई, उस अस्वाभाविक कामना के लिए खिसिया कर कहने लगी थी-"...पर मैं, क्या कभी ऐसा होने दूंगी! भले ही लाख अच्छे रिश्ते मिलें, वही होगा, जो हमारे कुल में सदा होता आया है। घर की बड़ी लड़की पहले विदा होगी, तब छोटी..."
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book









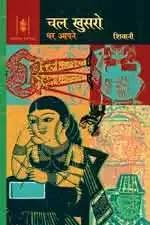


_s.webp)
