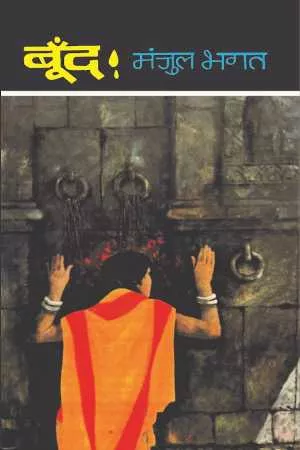|
कहानी संग्रह >> बूँद बूँदमंजुल भगत
|
176 पाठक हैं |
|||||||
कहानी संग्रह
Boond - A Hindi Book by - Manjul Bhagat - बूँद - मंजुल भगत
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
समकालीन हिन्दी कहानी की प्रतिष्ठित कथाकार मंजुल भगत की कहानियों के बारे में यह ठीक ही कहा गया है कि उनकी कहानियाँ धीमे से दस्तक देकर पाठक-मन में प्रवेश करती हैं और दबे-पाँव चुपचाप भीतर किसी कोने में दुबक कर बैठ जाती हैं। और फिर वहीं बसेरा करके रच बस जाती हैं। जब वे गायब होती हैं तो भी परछाई की तरह आसपास मंडराती रहती हैं - सूक्ष्म, सरल बनावट-बुनावट और बुनियादी सरोकारों के साथ।
मंजुल भगत के इस नवीनतम कहानी-संग्रह ‘बूँद’ में उसकी नयी कहानियाँ संग्रहीत हैं। चरित्रों की तटस्थ विश्लेषण, बिखरते मानव-मूल्यों के गम्भीर चिन्ता, जीवन और आसपास की व्यापक पृष्ठ भूमि तथा अनुभवों एवं संवेदनाओं की महीन अभिव्यक्ति इस संग्रह की कहानियों को पूरी सार्थकता के साथ अद्वितीय और विश्वसनीय बनाती हैं। ये कहानियाँ नारी के अभावों और संघर्षों से उपजी विद्रूपताओं, अर्थहीन रूढ़ियों और विसंगतियों की पड़ताल तो करती ही हैं, संस्कृति, संस्कार, परिवेश और चरित्रों का सम्रग भीतरी संसार भी अपने अन्दर समेटे हुए हैं।
मंजुल भगत के इस नवीनतम कहानी-संग्रह ‘बूँद’ में उसकी नयी कहानियाँ संग्रहीत हैं। चरित्रों की तटस्थ विश्लेषण, बिखरते मानव-मूल्यों के गम्भीर चिन्ता, जीवन और आसपास की व्यापक पृष्ठ भूमि तथा अनुभवों एवं संवेदनाओं की महीन अभिव्यक्ति इस संग्रह की कहानियों को पूरी सार्थकता के साथ अद्वितीय और विश्वसनीय बनाती हैं। ये कहानियाँ नारी के अभावों और संघर्षों से उपजी विद्रूपताओं, अर्थहीन रूढ़ियों और विसंगतियों की पड़ताल तो करती ही हैं, संस्कृति, संस्कार, परिवेश और चरित्रों का सम्रग भीतरी संसार भी अपने अन्दर समेटे हुए हैं।
बानो
उमस, पसीना और प्यास। सूरज तपकर ढल चुका था। गली हुई शाम यूँ ठहरी थी, मानो मोमबत्ती पिघलकर थक्कों में जमी हो। हवा के नाम पर अपनी साँसें थी।
टाइप और फोटोस्टेट के कार्यालय जाना आवश्यक हो गया। कुछ जरूरी आलेख थे जो हाथों-हाथ टंकित होने थे। बैठते ही कंठ लगा सूखने। ‘कनाडा ड्राई’ की ठण्डी बोतल मँगवाकार, घूँट-घूँट भरने लगी। सेबों के रस का अच्छा-सा पेय निकाला है। गला तर होने लगा पर माथे पर अब भी पसीना चुहचुहा रहा था। तभी उन्हें दूकान में दाखिल होते देखा। कुछ खब्तुलहवास-सी थीं।
‘‘बराये-मेहरबानी, मेरे कुल दो कागज पहले टाइप कर दें।’’
उनके ‘पहले’ शब्द पर मेरे कान खड़े हो गये। ‘‘देखिए, आपको अपनी बारी का इन्तजार करना होगा।’’ मैंने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा रगड़ते हुए कहा।
‘‘जी, मुझे दरअसल जाना था।’’
‘‘जाना तो खैर सभी को है। यहाँ रहने तो कोई नहीं आया।’’ मेरी आँखों का चश्मा पसीने से धुँधला गया था। आँखों के नीचे जहाँ पसीना इकट्ठा हो गया था, वहाँ चिरमिराहट होने लगी थी। मैंने चश्मा अतारकर पोंछा। दोबारा पहना तो उनका चेहरा इस कदर बुझा पाया कि मेरा मन कचोट उठा।
‘‘आइए। यहाँ सीफे पे बैठ लीजिए उतनी देर।’’
वह एकदम से मेरे करीब चली आयीं। चेहरे पर अब भी मायूसी पुती थी। बैठते ही पैर बदल-बदल के अपने पाँव छिपाने लगीं। पाँव छिपाने की बजाय और रोशनी में आ गये। बिवाई फटे, धूल अटे। किरमिची स्लीपरों में जहँ-तहाँ फटन और ढिलाई जिसमें पंजा आगे को सरका हुआ और स्लीपर पीछे फालतू निकला हुआ। मेरी चोर-नजर को पकड़ते हुए एकदम से बौखला गयीं।
‘‘आपा, मैं शुरू से ऐसी बेहाल न थी।’’
‘‘................।’’
‘‘वो तो दफ्तर जाते तो फैशनेबल खातूनों की चप्पलें देख-देख के मेरे लिए वैसी ही चप्पल खरीद लाते।’’
फिर वह अपना मैलखोर रंग का दुपट्टा ठीक करने लगीं।
‘‘साड़ी के अर्ज का ये लहीम-शहीम दुपट्टा मेरे लिए मोल ले आते। मैं चोटी खोल देती तो मेरे पुरपेंच बालों को बिखरा देते। कहते, इस लहर पर खुदा की खैर, बानो ! अब देख लीजिए मुझे, अबला-पा और खिचड़ी बाल।’’
उनकी आँखों में नमी का तार खिंच गया।
‘‘गुस्ले-सेहत के बाद मैं चोटी गूँथने बैठती तो हाथ से कंघी छीनकर खुद सँवार देते। चार-चार लटों की चोटी गूँथ, मोगरा तक टाँक देते।’’
उनकी आँखों का पानी मुसकाने लगा।
‘‘अपने साथ बाजार में खाना खिलाने ले जाते। दक्खनी खाना। प्लेट की शै देखकर मेरी पेशानी पे शिकन पड़ती, फौरन लड़के को टोक देते - ‘गोश्त का शोरबा दुरुस्त नहीं। ले जाओ उठाके। हम पूरी कीमत अदा करेंगे। पहले यखनी लेके आओ।’ हम कभी ऐसा-वैसा गोश्त न खाते...। समझ रही हैं न ? न ऐसा, न वैसा। फकत बकरे का।’’
न ! धूप में खड़ा नहीं होने देते मुझे। कहते, ‘नाहक अपनी सन्दली रंगत, धुँआ-धुँआ करे दे रही हो। हम जो हैं, बानो, बाहर का समेटने को।’ मैं हँस पड़ती। सोचती अपने-आप तो बिलकुल ही धूप-से उजले हैं और मेरी सोच पड़ी है। शौकीन ऐसे कि बन-सँवरकर हैदराबादी, गोल, गुम्मी टोपी पहन के जो निकल जाएँ तो गली जी उठे।
‘हीय !’ वह अचानक पीठ सीधी करके अपनी गरदन पकड़कर कराह उठीं। मेरे पूछने से अव्वल बोलीं –
‘‘जकड़ी पड़ी है। पुरानी सब्जी मण्डी के सामने, घण्टाघर के पास हनुमान पहलवान को पहचानती हैं आप ? वही, जो काला मलहम गरम करके, पट्टी पर फैला कर मरीज की गरदन पर बाँध देता है ? वहीं, मुझे ले चलते। बस, मोच-चनका सिरे से गायब। हम वहीं तो रहते थे, पुरानी दिल्ली में। वो गली नहीं है– बड़ी मशहूर-सी, जहाँ नूरा हज्जाम, जो जर्राह भी है, उसकी दूकान है। कैसा भी फोड़ा-फफोला हो, पहले तो पत्थर-तोड़ पत्ते को तवे पर गरम करके कड़ुआ तेल चुपड़ के उसपे बाँध दे। फिर जब फोड़ा बिना मुँह के पक ले तो इस सफाई से चीरा दे कि तमाम मवाद बाहर आ रहे। अरे, उस गली में तो ऐसे-ऐसे भी थे जो छुरा भोंक के निवाला तोड़ते थे। पर अपनी गली में सबसे मिसकोट किये रहते। कौआ, कौए का माँस नहीं खाता न।
आपा, चाँद-रात हो या अमावस काली चोर-रात, मैं अपनी ईद सजा ही लेती।
वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिला। अब तो जिन्दगी रुकी हुई चींटी-सी होके रह गयी है। उनके लिए तो मेरी भी जान हाजिर थी।
उनके दोस्त-अहबाब आते, तो मैं पसन्दे पकाती। वे कसाई-कस्साब से बकरे के गोश्त को छुरे से कजो के ले आते। मैं तब तक मसाले दही में भून लेती। मच्छी-अण्डे में प्याज-लहसुन और अदरक तो वे ही रगड़ के रख जाते। बस मैं पसन्दे भुने मसाले में डालकर खूब खिंचाई करती, जब तक दही और मक्खन किनारे न छोड़ दें। बस फिर भुने पसन्द समेटती जाती। साथ में मटर-मँगोरी का सालन। कोई एक साहब थे जो अगरचे-मगरचे के बगैर बात ही आगे न बढ़ा पाते। बस यह समझ लो आपा कि उनकी तो, अगरचे की रोटी, मगरचे की दाल, चुनाँचे की चटनी बड़ी ही मजेदार रहा करती।’’
आखिर बानो खिलखिला पड़ी। मैं भी हलकी पड़ गयी।
‘‘सच, बड़ी अनउलझी-सी खुशी हुआ करती। मेरी सास आयीं तो मैंने उनकी खिदमत में कुछ बाकी न उठा रखा। वो तो खाकर थाली भी परे को न सरकातीं। मैं ही उठा ले जाती। हाथ भी घण्टे बाद धोतीं। जाते-जाते सर्द-सी आह भरकर बोलीं, ‘क्या करें बानो, तुम मेरे जाँ-नशीन की मंजूर-नजर हो, नहीं तो पहलेवाली तो आला खानदान से थी।’ ’’
‘‘बस, मेरे किये-कराये को नाबदान में बहा दिया।’’
‘‘पहलेवाली ?’’
‘‘हाँ आँ, आपा। जिसमें उनकी जान थी, उसी को धक्के खिलवा दिये उनकी पहली बीवी ने तो। मोहल्लेवाले बताया करते कि गजब की झगड़ालू थीं। जो लिपट जाएँ तो दामन छुड़ाना मुश्किल। मुँहजोर बला की। मेरी नजर भी दो-चार हुई थी, उनसे। सुखाया हुआ, खजूर-सी थीं वे, एकदम छुआरा। झपटकर बोलीं, ‘तो आज एक आँख में सुरमा और दूसरी में धूल झोंक दी ?’ ’’
मैं तो खौफ खा गयी। उनसे सुहाग बाँट लेने को राजी हो गयी। सुनकर ये तुनक गये। बोले-
‘‘बात अपनी जगह है बानो। भला चाहत पे मोहर लगी है कभी ? पहली को कभी निभानी आयी ही नहीं हमसे। वस्ल की सरखुशी हमें उनसे कभी हासिल नहीं हुई। दिल की तहों से उन्होंने हमें कभी न चाहा। जब देखो तब हर किसी पर जंगली बिल्ली-सी झपट पड़तीं। बदसलीका थीं। उनके मायके में तो आगे दौलत, पीछे दौलत। तिस पर ऊँची जात, खान की बेटी। हमसे सातेक बरस बड़ी थीं। अब लचक तो कच्ची टहनी में ही होती है। उनके भाई-जान ने अपने ही नजरबाग में फरेब देके हमें फाँस लिया। शैतान से सौदा हो गया। रह लिए हम छह बरस उनकी मुलाजमत में। पहले तो कभी उनकी पतंग ही तुक में न रही, जब अपनी परछाईं पर पाँव पड़ा तो बिलख उठीं।’’
उनका भाई तो आकर दम दे गया।
‘‘बड़े-बड़े दाँतवाले बैठे हैं हमारे पीछे, एक ही नजर में ढेला हो जाओगे, दूल्हा-भाई।’’
ये भी ताव खा गये, बा-आवाज बुलन्द बोले –
‘‘क्यों ? खुदा आपका सगा लगता है क्या, जो अब रोड़े ऊपर उछलेंगे और ईंटें दब जाएँगी ? उखाड़कर फेक दूँगा, मूँछ भी और पूँछ भी। दुलदुल कहीं का।’’ पर कोई खुदाई ताकत हमारी दस्तगीरी कर रही थी। वह कबीलियत की घड़ी थी आपा।
बड़ी से तलाक हो गया और मुझसे निकाह। मैंने अपने मिट्टी के प्याले में चाँद उतार लिया।
वो कहा करते, तुम घबराना नहीं, बानो। हम तुम्हारी राहों में तमाम खार चुन के जाएँगे। तुम्हें लेकर अब हम, शामों को शमा जलायें या शामियाना लगवायें, उनसे मतलब ?
कुल पाँच बरस ही शामों को शमा जली होगी कि उन्होंने खाट पकड़ ली। हकीमों ने बहुतेरी माजून चटायी। इमामदस्ते में कूट-छानकर मैंने कितने ही नुस्खे आजमा लिये। ये हारते ही चले गये, बोले-
‘‘तबीयत गैर हुई जाती है, बानो। बेफायदा चारागिरी से अब कुछ ना होगा। चार पैसे अपनी खातिर बचा रक्खो।’’
मैं रात को उनके पहलू से उठ जाती तो मुझे टोहने लगते, कहते-
‘‘यूँ ना उठ जाया करो बानो, हमारा जी उलटने लगता है।’’
ये जी से गये, जान से गये। सब-कुछ सर्द-सर्द हो गया। उदासी पुर गयी मेरे घर-दालान में। काले साये चौमुहानी तक पसर गये। ये तो देखो आपा, जो शौहर की मय्यत तक में शरीक न हुई वह अपना हक-हिसाब माँगने आ पहुँची। बड़ी ने तो मेहर में उनका नूरे-चश्म तक माँग लिया था। वह भी बाप की मिट्टी समेटने ना पहुँचा। एक ही अण्डा, वो भी गन्दा। तुम तो पहले ही मालों में थी बड़ी, फिर मेरे खाने-
खर्चे पे हाथ क्यों डाला ? यह तो बतलाओ मेरी अच्छी आपा, कि मेरा बच्चा क्यों नहीं हुआ उनसे ?
बड़ी के भाई ने, जरूरी कागजात से भरी मेरी अटैची, चोरी करवा ली, एक सन्दूकचू भी उड़वा ली, जिसमें मेरी वे दो पोशाकें थीं जिन्हें उन्होंने शौक से बनवा कर दी थीं। एक नौबहार सब्ज और दूसरी आतिशी सुर्ख। कलाबत्तू में पिरोयी हुई कुन्दन की टुकड़ियाँ भी थीं।
बड़ी कानों में गूँजनेवाली अजान भूल गयीं। पर दगा किसी की सगी नहीं होती। मैंने भी मुकदमा ठोंक दिया। काँटे से ही काँटा निकाला जाता है, आपा। तभी तो कागज लिए रास्ते की धूल फाँक रही हूँ। दावे जवाबी दावों की दरख्वास्तें चल रहीं हैं। बस दिन-भर वकालत-अदालत और रात-पड़े खुली आँख अँधेरा पीना। अभी कल ही उस पुरानी गली से गुजरी तो आज तलक रोटी को कौर न तोड़ा गया। शीला बाजी ने अगर मुझे समेट न लिया होता, तो न जाने क्या हो रहता ?
शेखूपुरा में उनके ही साथ रहती हूँ। पिछले मकान से तो उन लोगों ने खदेड़ ही दिया था, खुदा के पिछवाड़े। शीला बाजी तो कहती हैं, ‘‘यही कुछ होता है बानो, सुन्दर हुनरमन्द लड़कियाँ गली-गली घूमें और कर्कशा बेशऊर राज राजें।’’ कहती हैं, ‘‘क्या हिन्दू और क्या मुसलमान। कोस-कोस पर बदले पानी और चार कोस पे बानी। हमारे यहाँ पावन तुलसी तो तुम्हारे यहां वहीं जन्मत का पौधा।’’ शीला बाजी तो अच्छे वक्तों में, हजरतबल की मस्जिद में दुआ भी माँग आयीं जाके।
मेरे वालिद आजादी के सिपाही थे, स्वतंत्रता-सेनानी। उनके साथ मेरी तस्वीरें जो थीं। सो जब सन् उन्नीस सौ बयालीस से लेकर उन्नीस सौ बानवे तक, पचास बरस हो गये, तब सरकार से यह तमगा मिला है मुझे। यह देखो, अब्बा-हुजूर का नाम खुदा है इसपे। और यह रहा मेरा सरकारी बस-पास। इसकी बदौलत मैं जमाने की खाक छान सकती हूँ। एक हमशीरा भी थी मेरी। मुझसे दो-एक बरस छोटी, बन्नो। हम दोनों की सूरत यकसाँ थी। बस, एक को उठा दो। बड़ी याद आती है
उसकी। जाने कहाँ गुम है ? अच्छे घर ब्याही थी। खुदा की राह पे हूँ आपा, झूठ नहीं बोलूँगी शीला बाजी, कमके का किराया तक नहीं लेतीं मुझसे। कहती हैं–‘‘बानो, यो रोने-रुलाने से क्या बनेगा ?’’ हाँ, आपा, हिम्मते-मुरदा, मददे खुदा। यह औरत पे ही ज्यादा खरा उतरता है। कुछ कसीदाकारी कर लेती हूँ। तुरपाई-टँकाई भी। रफूगर भी। अच्छी हूँ। बस, गुजारे के पैसे आ जाते हैं।
अरे ! हो भी लिए आपके कागजात ? मेरे हो लें तो चलूँ। शीला बाजी फिक्रमन्द हो आती हैं, मैं कहीँ अटक-भटक जाऊँ तो।
लाहौल बिला-कूवत इल्ला बिल्ला
लाहौल-बिल अजीम।...
ये कैसी बेपर्द तर्ज छिड़ी है बगल के रेड़ियो पर ? बोल तो न सुने जाएँ, न अनसुने किये जाएँ। यों तो मिरासिने गाया करती हैं। दुरुस्त हो गये तुम्हारे कागजात ? ये तुम्हारा खलूस ही है, बीवी, जिसने एक ही मुलाकात में सब उगलवा लिया। लगता है, आज तो टूट के बरसेगा पानी।
मुद्दतों बाद किसी ने हाले-दिल सुना है।
बानो के कागज टाइप होने शुरू हो गये थे।
पर यह आसमान को क्या हुआ ? उमड़-घुमड़ के इस तौर बरसा जैसे पहले कभी बरसा ही न हो।
दो–एक बार फिर भी टाइप स्कूल में जाना हुआ। लगा था, अभी के अभी बानो कहीं से नमूदार हो जाएगी। पर ऐसा न हुआ। उनका अता-पता ले लिया होता। वे शेखूपुरी में रहती हैं खाली, यह जान लेने से क्या होता-जाता है ? पर, गैरों के पते दर्ज किये जाते हैं कहीं ? अपना ही दे आती। गैर को अपने मकान का पता भी तो नहीं जतलाया जाता। छोड़ो फिर, यह कुरेद-सी काहे लगी है, कि बस उनसे सामना हो जाए ? आखिर मैं कार्यालय में अपना पता छोड़ ही आयी कि वह आयें तो मेरे यहाँ भेज दें।
बानो नहीं आयीं। आये तो एक साहब। दरियाफ्त करने लगे –
‘‘मेरी वालिदा क्या आपके पास आयी थीं ?’’
‘‘आपकी तारीफ ?’’
‘‘जी मैं अनवर हूँ।’’
‘‘...........’’
‘‘जी, आपका पता, टाइप-स्कूलवालों ने दिया है। मेरी वालिदा वहाँ जाया करती थीं, कचहरी के लिए अपने कागजात के कील-काँटे दुरुस्त करवाने, मकदमे-पेशी के चलते।’’
मैं जरा-सी चौंकी, फिर कुछ उत्सुकता से पूछा, ‘‘उनका नाम ?’’
‘‘जी, बानो। वैसे पूरा नाम तो गुलबानो था पर सब बानो ही पुकारा करते।’’
‘‘मगर वो कहती थीं कि उनके कोई औलाद हुई ही नहीं ?’’
‘‘ऐसा कहा क्या उन्होंने ? उस दूसरे शौहर गुलशेर से न हुई होगी। जी, मेरे अब्बा तो उनके पहले खाविन्द थे।’’
‘‘खैर। बानो यहाँ कभी नहीं आयीं। अगर आ ही जाएँ तो भला क्या कह दूँ ?’’
‘‘यही...कि वो फौरन बल्लीमारान चली आएँ, बड़े भाई साहब के यहाँ।’’
‘‘अच्छा....अच्छा। आपके भाईसाहब शायद आपके वालिद की पहली बीवी से होंगे ?’’
अजी तौबा बोलिए। हम सगे भाई हैं और गुलबानो हमारी सगी अम्मी। मैं दरअसल मझले भाई के साथ उनके शेखूपुरावाले ठिकाने पे होके आया था। पर कोई नतीजा न निकला।’’
‘‘मझले भाई ?’’
‘‘जी, वही। छुट्टन यानी छोटे भी वहाँ के तीन-चार चक्कर लगा आया। लगता है, वह हमसे छिप रही हैं।’’
‘‘ये छोटे आपके वालिद की दूसरी बेगम से होंगे ? क्योंकि बानो अपनी आपबीती मुझसे एक-साँस बयान कर चुकी थीं, मेरा इतना पूछ लेना मुनासिब ही था।’’
‘‘ना...न...हम सब सगे भाई हैं। अब्बाहुजूर ने तो कुल जमा एक ही मर्तबा सेहरा पहना था।’’
‘‘हम सब ?’’
‘‘जी, खुदा के फजल से हम चार भाई हैं।’’
मेरे जेहान में बानो का सुता-सुताया, इकहरा जिस्म घूम गया। मेके चेहरे पर पुते अचरज को देख अनवर ने सफाई पेश की-
‘‘ऐसी बात नहीं है। अब्बाहुजूर अम्मी को हर जच्चगी के लिए मछलीवाले शफाखाने ले जाते थे।’’
‘‘मगर तुम लोगों के रहते बानो क्यों यहाँ-वहाँ की धूल समेट रही हैं ?’’
‘‘देखिए, दिलों में तो हमारे फर्क आना चाहिए था। वे चार-चार बेटे-बहुओं से किनारा-कशी कर, किसी गैर के पहलू में जा बैठीं। यहाँ तक कि उस शख्स, गुलशेर के इन्तकाल के बाद भी अम्मी हम लोगों से ऐंठी रहीं, बेसबब, बेमतलब।’’
‘‘बेसबब तो खैर कुछ भी नहीं होता।’’
‘‘इस कदर शर्मिन्दा हुए हम लोग कि क्या कहें। हमारी अम्मी और ये बेजा हरकत, उम्र के इस पड़ाव पर ?’’
‘‘खुशी हासिल करने का हक तो सभी रखते हैं ?’’
‘‘खुशी ? अल्लाह मियाँ के नजदीक खिदमत अहमियत रखती है, जनाब। दो वक्तों की रोटी तो उन्हें हमारे वहाँ भी नसीब थी। सलमानी हैं हम लोग। हेयर कटिंग सैलून चलता है हमारा। पेशेवर हज्जाम हैं। आखिर हम भी आस-औलादवाले थे। पोतों-पोतड़ों में बैठी अम्मी दिखलाई भी न पड़तीं। हमारी बीवियाँ तो सभी बच्चों को उन्हीं के सुपुर्द किये रहतीं खिलाये जाओ जी भरके। और कैसी मसर्रत चाहिए औरत को, वो भी उम्र के इस दौर में ?’’
‘‘......................’’
‘‘मैं कुबूल करता हूँ कि उम्र-भर अम्मी हमें बड़ा करने में लगी रहीं। अब्बा तो कह दिया करते, नसीबोंवाली है, बेटे-ही-बेटे जने हैं। तेरा अपना ही पेट, पड़ी-पड़ी समेट।
जब अब्बा के तपेदिक से खाट पकड़ ली तब अम्मी ने रात-दिन एक करके खिदमत की, किसी नेक बीवी की तरह। उसका सवाब भी तो उन्हीं को मिलेगा। उन्हें तो खबर ही न होती कब आफताब उरूज होता और कब गरूब। कब आसमाँ अपने रंग बदलता। जाने कब अम्मी बालों में कंघी देतीं। बस अब्बा की खाँसी बलगम और उगालदान। घर के गोशे-गोशे से अम्मी की बुलाहट गूँजती रहती। अब कह तो दीजिए कि हमारे वहाँ अम्मी की पूछ न थी ? जब गयीं तो नन्हे-बाँके तो दिनोंदिन उनका हेरूआ करते रह गये। बच्चे भी ऐसे कि अण्डे में से निकलते ही बाँग देना शुरू। तमाम दिन बवाल मचाये रखते। अम्मी का ही बूता था कि उन्हें दबोचे-समेटे रखतीं। तमाम दिन बवाल मचाये रखतीं। आखिर दादीजान थीं न।’’
अनवर हँस रहा था कि हिनहिना रहा था, वही जाने।
‘‘हमारी बीवियाँ तो उनकी पकायी, हाँडी-दगेची भुलाये न भूलतीं। पूरा बावर्चीखाना जो उनके सुपुर्द था। अब भी कह देंगी, अपनी अम्मी को ही खोज के ले आओ। कुनबा-परवर देग को घुमा-फिरा के आँच देना, आटे से घेर बाँध के घण्टों गरमाये रखना, ये सब उन्हीं के बस की बात थी। अब्बा के गुजर जाने के बाद तो हम लोग अम्मी को और भी उलझाये रखते कि वे नाहक उनकी याद में जी छोटा न किये रहें। मेरी बीवी तो आप जानिए, जरा भी दखल-अन्दाजी न करती। यूँ भी बेहद खुशमिजाज है, बस पान खाना हँसते रहना।’’ इस बार अनवर गुदगुदाया-सा हँस दिया।
‘‘सच में, अम्मी को कोई टोकनेवाला न था। अम्मी तो तिराहे पर से रसद तक उठवा लातीं। हमारी तो परदें में रहतीं। बस, यूँही, तिराहे-चौराहे पे मुलाकात हो गयी होगी उस शख्स से। बखिया उधेड़ के रख दी हमारी।
खैर ! अम्मी आयें तो भेज दीजिएगा। कहिएगा, उनकी बहुएँ भी तो अब कहाँ इतनी कड़ियल-जवान रह गयी हैं। आखिर औरत को औरत का ही सहारा होता है। तो बीबी, अब इजाजत दें। सलाम।’’
‘‘सलाम !’’–मैं उस शख्स की लौटती पीठ ताकती रह गयी जो बानो का पेट-जाया था, अपना था, सगा था।
टाइप और फोटोस्टेट के कार्यालय जाना आवश्यक हो गया। कुछ जरूरी आलेख थे जो हाथों-हाथ टंकित होने थे। बैठते ही कंठ लगा सूखने। ‘कनाडा ड्राई’ की ठण्डी बोतल मँगवाकार, घूँट-घूँट भरने लगी। सेबों के रस का अच्छा-सा पेय निकाला है। गला तर होने लगा पर माथे पर अब भी पसीना चुहचुहा रहा था। तभी उन्हें दूकान में दाखिल होते देखा। कुछ खब्तुलहवास-सी थीं।
‘‘बराये-मेहरबानी, मेरे कुल दो कागज पहले टाइप कर दें।’’
उनके ‘पहले’ शब्द पर मेरे कान खड़े हो गये। ‘‘देखिए, आपको अपनी बारी का इन्तजार करना होगा।’’ मैंने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा रगड़ते हुए कहा।
‘‘जी, मुझे दरअसल जाना था।’’
‘‘जाना तो खैर सभी को है। यहाँ रहने तो कोई नहीं आया।’’ मेरी आँखों का चश्मा पसीने से धुँधला गया था। आँखों के नीचे जहाँ पसीना इकट्ठा हो गया था, वहाँ चिरमिराहट होने लगी थी। मैंने चश्मा अतारकर पोंछा। दोबारा पहना तो उनका चेहरा इस कदर बुझा पाया कि मेरा मन कचोट उठा।
‘‘आइए। यहाँ सीफे पे बैठ लीजिए उतनी देर।’’
वह एकदम से मेरे करीब चली आयीं। चेहरे पर अब भी मायूसी पुती थी। बैठते ही पैर बदल-बदल के अपने पाँव छिपाने लगीं। पाँव छिपाने की बजाय और रोशनी में आ गये। बिवाई फटे, धूल अटे। किरमिची स्लीपरों में जहँ-तहाँ फटन और ढिलाई जिसमें पंजा आगे को सरका हुआ और स्लीपर पीछे फालतू निकला हुआ। मेरी चोर-नजर को पकड़ते हुए एकदम से बौखला गयीं।
‘‘आपा, मैं शुरू से ऐसी बेहाल न थी।’’
‘‘................।’’
‘‘वो तो दफ्तर जाते तो फैशनेबल खातूनों की चप्पलें देख-देख के मेरे लिए वैसी ही चप्पल खरीद लाते।’’
फिर वह अपना मैलखोर रंग का दुपट्टा ठीक करने लगीं।
‘‘साड़ी के अर्ज का ये लहीम-शहीम दुपट्टा मेरे लिए मोल ले आते। मैं चोटी खोल देती तो मेरे पुरपेंच बालों को बिखरा देते। कहते, इस लहर पर खुदा की खैर, बानो ! अब देख लीजिए मुझे, अबला-पा और खिचड़ी बाल।’’
उनकी आँखों में नमी का तार खिंच गया।
‘‘गुस्ले-सेहत के बाद मैं चोटी गूँथने बैठती तो हाथ से कंघी छीनकर खुद सँवार देते। चार-चार लटों की चोटी गूँथ, मोगरा तक टाँक देते।’’
उनकी आँखों का पानी मुसकाने लगा।
‘‘अपने साथ बाजार में खाना खिलाने ले जाते। दक्खनी खाना। प्लेट की शै देखकर मेरी पेशानी पे शिकन पड़ती, फौरन लड़के को टोक देते - ‘गोश्त का शोरबा दुरुस्त नहीं। ले जाओ उठाके। हम पूरी कीमत अदा करेंगे। पहले यखनी लेके आओ।’ हम कभी ऐसा-वैसा गोश्त न खाते...। समझ रही हैं न ? न ऐसा, न वैसा। फकत बकरे का।’’
न ! धूप में खड़ा नहीं होने देते मुझे। कहते, ‘नाहक अपनी सन्दली रंगत, धुँआ-धुँआ करे दे रही हो। हम जो हैं, बानो, बाहर का समेटने को।’ मैं हँस पड़ती। सोचती अपने-आप तो बिलकुल ही धूप-से उजले हैं और मेरी सोच पड़ी है। शौकीन ऐसे कि बन-सँवरकर हैदराबादी, गोल, गुम्मी टोपी पहन के जो निकल जाएँ तो गली जी उठे।
‘हीय !’ वह अचानक पीठ सीधी करके अपनी गरदन पकड़कर कराह उठीं। मेरे पूछने से अव्वल बोलीं –
‘‘जकड़ी पड़ी है। पुरानी सब्जी मण्डी के सामने, घण्टाघर के पास हनुमान पहलवान को पहचानती हैं आप ? वही, जो काला मलहम गरम करके, पट्टी पर फैला कर मरीज की गरदन पर बाँध देता है ? वहीं, मुझे ले चलते। बस, मोच-चनका सिरे से गायब। हम वहीं तो रहते थे, पुरानी दिल्ली में। वो गली नहीं है– बड़ी मशहूर-सी, जहाँ नूरा हज्जाम, जो जर्राह भी है, उसकी दूकान है। कैसा भी फोड़ा-फफोला हो, पहले तो पत्थर-तोड़ पत्ते को तवे पर गरम करके कड़ुआ तेल चुपड़ के उसपे बाँध दे। फिर जब फोड़ा बिना मुँह के पक ले तो इस सफाई से चीरा दे कि तमाम मवाद बाहर आ रहे। अरे, उस गली में तो ऐसे-ऐसे भी थे जो छुरा भोंक के निवाला तोड़ते थे। पर अपनी गली में सबसे मिसकोट किये रहते। कौआ, कौए का माँस नहीं खाता न।
आपा, चाँद-रात हो या अमावस काली चोर-रात, मैं अपनी ईद सजा ही लेती।
वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिला। अब तो जिन्दगी रुकी हुई चींटी-सी होके रह गयी है। उनके लिए तो मेरी भी जान हाजिर थी।
उनके दोस्त-अहबाब आते, तो मैं पसन्दे पकाती। वे कसाई-कस्साब से बकरे के गोश्त को छुरे से कजो के ले आते। मैं तब तक मसाले दही में भून लेती। मच्छी-अण्डे में प्याज-लहसुन और अदरक तो वे ही रगड़ के रख जाते। बस मैं पसन्दे भुने मसाले में डालकर खूब खिंचाई करती, जब तक दही और मक्खन किनारे न छोड़ दें। बस फिर भुने पसन्द समेटती जाती। साथ में मटर-मँगोरी का सालन। कोई एक साहब थे जो अगरचे-मगरचे के बगैर बात ही आगे न बढ़ा पाते। बस यह समझ लो आपा कि उनकी तो, अगरचे की रोटी, मगरचे की दाल, चुनाँचे की चटनी बड़ी ही मजेदार रहा करती।’’
आखिर बानो खिलखिला पड़ी। मैं भी हलकी पड़ गयी।
‘‘सच, बड़ी अनउलझी-सी खुशी हुआ करती। मेरी सास आयीं तो मैंने उनकी खिदमत में कुछ बाकी न उठा रखा। वो तो खाकर थाली भी परे को न सरकातीं। मैं ही उठा ले जाती। हाथ भी घण्टे बाद धोतीं। जाते-जाते सर्द-सी आह भरकर बोलीं, ‘क्या करें बानो, तुम मेरे जाँ-नशीन की मंजूर-नजर हो, नहीं तो पहलेवाली तो आला खानदान से थी।’ ’’
‘‘बस, मेरे किये-कराये को नाबदान में बहा दिया।’’
‘‘पहलेवाली ?’’
‘‘हाँ आँ, आपा। जिसमें उनकी जान थी, उसी को धक्के खिलवा दिये उनकी पहली बीवी ने तो। मोहल्लेवाले बताया करते कि गजब की झगड़ालू थीं। जो लिपट जाएँ तो दामन छुड़ाना मुश्किल। मुँहजोर बला की। मेरी नजर भी दो-चार हुई थी, उनसे। सुखाया हुआ, खजूर-सी थीं वे, एकदम छुआरा। झपटकर बोलीं, ‘तो आज एक आँख में सुरमा और दूसरी में धूल झोंक दी ?’ ’’
मैं तो खौफ खा गयी। उनसे सुहाग बाँट लेने को राजी हो गयी। सुनकर ये तुनक गये। बोले-
‘‘बात अपनी जगह है बानो। भला चाहत पे मोहर लगी है कभी ? पहली को कभी निभानी आयी ही नहीं हमसे। वस्ल की सरखुशी हमें उनसे कभी हासिल नहीं हुई। दिल की तहों से उन्होंने हमें कभी न चाहा। जब देखो तब हर किसी पर जंगली बिल्ली-सी झपट पड़तीं। बदसलीका थीं। उनके मायके में तो आगे दौलत, पीछे दौलत। तिस पर ऊँची जात, खान की बेटी। हमसे सातेक बरस बड़ी थीं। अब लचक तो कच्ची टहनी में ही होती है। उनके भाई-जान ने अपने ही नजरबाग में फरेब देके हमें फाँस लिया। शैतान से सौदा हो गया। रह लिए हम छह बरस उनकी मुलाजमत में। पहले तो कभी उनकी पतंग ही तुक में न रही, जब अपनी परछाईं पर पाँव पड़ा तो बिलख उठीं।’’
उनका भाई तो आकर दम दे गया।
‘‘बड़े-बड़े दाँतवाले बैठे हैं हमारे पीछे, एक ही नजर में ढेला हो जाओगे, दूल्हा-भाई।’’
ये भी ताव खा गये, बा-आवाज बुलन्द बोले –
‘‘क्यों ? खुदा आपका सगा लगता है क्या, जो अब रोड़े ऊपर उछलेंगे और ईंटें दब जाएँगी ? उखाड़कर फेक दूँगा, मूँछ भी और पूँछ भी। दुलदुल कहीं का।’’ पर कोई खुदाई ताकत हमारी दस्तगीरी कर रही थी। वह कबीलियत की घड़ी थी आपा।
बड़ी से तलाक हो गया और मुझसे निकाह। मैंने अपने मिट्टी के प्याले में चाँद उतार लिया।
वो कहा करते, तुम घबराना नहीं, बानो। हम तुम्हारी राहों में तमाम खार चुन के जाएँगे। तुम्हें लेकर अब हम, शामों को शमा जलायें या शामियाना लगवायें, उनसे मतलब ?
कुल पाँच बरस ही शामों को शमा जली होगी कि उन्होंने खाट पकड़ ली। हकीमों ने बहुतेरी माजून चटायी। इमामदस्ते में कूट-छानकर मैंने कितने ही नुस्खे आजमा लिये। ये हारते ही चले गये, बोले-
‘‘तबीयत गैर हुई जाती है, बानो। बेफायदा चारागिरी से अब कुछ ना होगा। चार पैसे अपनी खातिर बचा रक्खो।’’
मैं रात को उनके पहलू से उठ जाती तो मुझे टोहने लगते, कहते-
‘‘यूँ ना उठ जाया करो बानो, हमारा जी उलटने लगता है।’’
ये जी से गये, जान से गये। सब-कुछ सर्द-सर्द हो गया। उदासी पुर गयी मेरे घर-दालान में। काले साये चौमुहानी तक पसर गये। ये तो देखो आपा, जो शौहर की मय्यत तक में शरीक न हुई वह अपना हक-हिसाब माँगने आ पहुँची। बड़ी ने तो मेहर में उनका नूरे-चश्म तक माँग लिया था। वह भी बाप की मिट्टी समेटने ना पहुँचा। एक ही अण्डा, वो भी गन्दा। तुम तो पहले ही मालों में थी बड़ी, फिर मेरे खाने-
खर्चे पे हाथ क्यों डाला ? यह तो बतलाओ मेरी अच्छी आपा, कि मेरा बच्चा क्यों नहीं हुआ उनसे ?
बड़ी के भाई ने, जरूरी कागजात से भरी मेरी अटैची, चोरी करवा ली, एक सन्दूकचू भी उड़वा ली, जिसमें मेरी वे दो पोशाकें थीं जिन्हें उन्होंने शौक से बनवा कर दी थीं। एक नौबहार सब्ज और दूसरी आतिशी सुर्ख। कलाबत्तू में पिरोयी हुई कुन्दन की टुकड़ियाँ भी थीं।
बड़ी कानों में गूँजनेवाली अजान भूल गयीं। पर दगा किसी की सगी नहीं होती। मैंने भी मुकदमा ठोंक दिया। काँटे से ही काँटा निकाला जाता है, आपा। तभी तो कागज लिए रास्ते की धूल फाँक रही हूँ। दावे जवाबी दावों की दरख्वास्तें चल रहीं हैं। बस दिन-भर वकालत-अदालत और रात-पड़े खुली आँख अँधेरा पीना। अभी कल ही उस पुरानी गली से गुजरी तो आज तलक रोटी को कौर न तोड़ा गया। शीला बाजी ने अगर मुझे समेट न लिया होता, तो न जाने क्या हो रहता ?
शेखूपुरा में उनके ही साथ रहती हूँ। पिछले मकान से तो उन लोगों ने खदेड़ ही दिया था, खुदा के पिछवाड़े। शीला बाजी तो कहती हैं, ‘‘यही कुछ होता है बानो, सुन्दर हुनरमन्द लड़कियाँ गली-गली घूमें और कर्कशा बेशऊर राज राजें।’’ कहती हैं, ‘‘क्या हिन्दू और क्या मुसलमान। कोस-कोस पर बदले पानी और चार कोस पे बानी। हमारे यहाँ पावन तुलसी तो तुम्हारे यहां वहीं जन्मत का पौधा।’’ शीला बाजी तो अच्छे वक्तों में, हजरतबल की मस्जिद में दुआ भी माँग आयीं जाके।
मेरे वालिद आजादी के सिपाही थे, स्वतंत्रता-सेनानी। उनके साथ मेरी तस्वीरें जो थीं। सो जब सन् उन्नीस सौ बयालीस से लेकर उन्नीस सौ बानवे तक, पचास बरस हो गये, तब सरकार से यह तमगा मिला है मुझे। यह देखो, अब्बा-हुजूर का नाम खुदा है इसपे। और यह रहा मेरा सरकारी बस-पास। इसकी बदौलत मैं जमाने की खाक छान सकती हूँ। एक हमशीरा भी थी मेरी। मुझसे दो-एक बरस छोटी, बन्नो। हम दोनों की सूरत यकसाँ थी। बस, एक को उठा दो। बड़ी याद आती है
उसकी। जाने कहाँ गुम है ? अच्छे घर ब्याही थी। खुदा की राह पे हूँ आपा, झूठ नहीं बोलूँगी शीला बाजी, कमके का किराया तक नहीं लेतीं मुझसे। कहती हैं–‘‘बानो, यो रोने-रुलाने से क्या बनेगा ?’’ हाँ, आपा, हिम्मते-मुरदा, मददे खुदा। यह औरत पे ही ज्यादा खरा उतरता है। कुछ कसीदाकारी कर लेती हूँ। तुरपाई-टँकाई भी। रफूगर भी। अच्छी हूँ। बस, गुजारे के पैसे आ जाते हैं।
अरे ! हो भी लिए आपके कागजात ? मेरे हो लें तो चलूँ। शीला बाजी फिक्रमन्द हो आती हैं, मैं कहीँ अटक-भटक जाऊँ तो।
लाहौल बिला-कूवत इल्ला बिल्ला
लाहौल-बिल अजीम।...
ये कैसी बेपर्द तर्ज छिड़ी है बगल के रेड़ियो पर ? बोल तो न सुने जाएँ, न अनसुने किये जाएँ। यों तो मिरासिने गाया करती हैं। दुरुस्त हो गये तुम्हारे कागजात ? ये तुम्हारा खलूस ही है, बीवी, जिसने एक ही मुलाकात में सब उगलवा लिया। लगता है, आज तो टूट के बरसेगा पानी।
मुद्दतों बाद किसी ने हाले-दिल सुना है।
बानो के कागज टाइप होने शुरू हो गये थे।
पर यह आसमान को क्या हुआ ? उमड़-घुमड़ के इस तौर बरसा जैसे पहले कभी बरसा ही न हो।
दो–एक बार फिर भी टाइप स्कूल में जाना हुआ। लगा था, अभी के अभी बानो कहीं से नमूदार हो जाएगी। पर ऐसा न हुआ। उनका अता-पता ले लिया होता। वे शेखूपुरी में रहती हैं खाली, यह जान लेने से क्या होता-जाता है ? पर, गैरों के पते दर्ज किये जाते हैं कहीं ? अपना ही दे आती। गैर को अपने मकान का पता भी तो नहीं जतलाया जाता। छोड़ो फिर, यह कुरेद-सी काहे लगी है, कि बस उनसे सामना हो जाए ? आखिर मैं कार्यालय में अपना पता छोड़ ही आयी कि वह आयें तो मेरे यहाँ भेज दें।
बानो नहीं आयीं। आये तो एक साहब। दरियाफ्त करने लगे –
‘‘मेरी वालिदा क्या आपके पास आयी थीं ?’’
‘‘आपकी तारीफ ?’’
‘‘जी मैं अनवर हूँ।’’
‘‘...........’’
‘‘जी, आपका पता, टाइप-स्कूलवालों ने दिया है। मेरी वालिदा वहाँ जाया करती थीं, कचहरी के लिए अपने कागजात के कील-काँटे दुरुस्त करवाने, मकदमे-पेशी के चलते।’’
मैं जरा-सी चौंकी, फिर कुछ उत्सुकता से पूछा, ‘‘उनका नाम ?’’
‘‘जी, बानो। वैसे पूरा नाम तो गुलबानो था पर सब बानो ही पुकारा करते।’’
‘‘मगर वो कहती थीं कि उनके कोई औलाद हुई ही नहीं ?’’
‘‘ऐसा कहा क्या उन्होंने ? उस दूसरे शौहर गुलशेर से न हुई होगी। जी, मेरे अब्बा तो उनके पहले खाविन्द थे।’’
‘‘खैर। बानो यहाँ कभी नहीं आयीं। अगर आ ही जाएँ तो भला क्या कह दूँ ?’’
‘‘यही...कि वो फौरन बल्लीमारान चली आएँ, बड़े भाई साहब के यहाँ।’’
‘‘अच्छा....अच्छा। आपके भाईसाहब शायद आपके वालिद की पहली बीवी से होंगे ?’’
अजी तौबा बोलिए। हम सगे भाई हैं और गुलबानो हमारी सगी अम्मी। मैं दरअसल मझले भाई के साथ उनके शेखूपुरावाले ठिकाने पे होके आया था। पर कोई नतीजा न निकला।’’
‘‘मझले भाई ?’’
‘‘जी, वही। छुट्टन यानी छोटे भी वहाँ के तीन-चार चक्कर लगा आया। लगता है, वह हमसे छिप रही हैं।’’
‘‘ये छोटे आपके वालिद की दूसरी बेगम से होंगे ? क्योंकि बानो अपनी आपबीती मुझसे एक-साँस बयान कर चुकी थीं, मेरा इतना पूछ लेना मुनासिब ही था।’’
‘‘ना...न...हम सब सगे भाई हैं। अब्बाहुजूर ने तो कुल जमा एक ही मर्तबा सेहरा पहना था।’’
‘‘हम सब ?’’
‘‘जी, खुदा के फजल से हम चार भाई हैं।’’
मेरे जेहान में बानो का सुता-सुताया, इकहरा जिस्म घूम गया। मेके चेहरे पर पुते अचरज को देख अनवर ने सफाई पेश की-
‘‘ऐसी बात नहीं है। अब्बाहुजूर अम्मी को हर जच्चगी के लिए मछलीवाले शफाखाने ले जाते थे।’’
‘‘मगर तुम लोगों के रहते बानो क्यों यहाँ-वहाँ की धूल समेट रही हैं ?’’
‘‘देखिए, दिलों में तो हमारे फर्क आना चाहिए था। वे चार-चार बेटे-बहुओं से किनारा-कशी कर, किसी गैर के पहलू में जा बैठीं। यहाँ तक कि उस शख्स, गुलशेर के इन्तकाल के बाद भी अम्मी हम लोगों से ऐंठी रहीं, बेसबब, बेमतलब।’’
‘‘बेसबब तो खैर कुछ भी नहीं होता।’’
‘‘इस कदर शर्मिन्दा हुए हम लोग कि क्या कहें। हमारी अम्मी और ये बेजा हरकत, उम्र के इस पड़ाव पर ?’’
‘‘खुशी हासिल करने का हक तो सभी रखते हैं ?’’
‘‘खुशी ? अल्लाह मियाँ के नजदीक खिदमत अहमियत रखती है, जनाब। दो वक्तों की रोटी तो उन्हें हमारे वहाँ भी नसीब थी। सलमानी हैं हम लोग। हेयर कटिंग सैलून चलता है हमारा। पेशेवर हज्जाम हैं। आखिर हम भी आस-औलादवाले थे। पोतों-पोतड़ों में बैठी अम्मी दिखलाई भी न पड़तीं। हमारी बीवियाँ तो सभी बच्चों को उन्हीं के सुपुर्द किये रहतीं खिलाये जाओ जी भरके। और कैसी मसर्रत चाहिए औरत को, वो भी उम्र के इस दौर में ?’’
‘‘......................’’
‘‘मैं कुबूल करता हूँ कि उम्र-भर अम्मी हमें बड़ा करने में लगी रहीं। अब्बा तो कह दिया करते, नसीबोंवाली है, बेटे-ही-बेटे जने हैं। तेरा अपना ही पेट, पड़ी-पड़ी समेट।
जब अब्बा के तपेदिक से खाट पकड़ ली तब अम्मी ने रात-दिन एक करके खिदमत की, किसी नेक बीवी की तरह। उसका सवाब भी तो उन्हीं को मिलेगा। उन्हें तो खबर ही न होती कब आफताब उरूज होता और कब गरूब। कब आसमाँ अपने रंग बदलता। जाने कब अम्मी बालों में कंघी देतीं। बस अब्बा की खाँसी बलगम और उगालदान। घर के गोशे-गोशे से अम्मी की बुलाहट गूँजती रहती। अब कह तो दीजिए कि हमारे वहाँ अम्मी की पूछ न थी ? जब गयीं तो नन्हे-बाँके तो दिनोंदिन उनका हेरूआ करते रह गये। बच्चे भी ऐसे कि अण्डे में से निकलते ही बाँग देना शुरू। तमाम दिन बवाल मचाये रखते। अम्मी का ही बूता था कि उन्हें दबोचे-समेटे रखतीं। तमाम दिन बवाल मचाये रखतीं। आखिर दादीजान थीं न।’’
अनवर हँस रहा था कि हिनहिना रहा था, वही जाने।
‘‘हमारी बीवियाँ तो उनकी पकायी, हाँडी-दगेची भुलाये न भूलतीं। पूरा बावर्चीखाना जो उनके सुपुर्द था। अब भी कह देंगी, अपनी अम्मी को ही खोज के ले आओ। कुनबा-परवर देग को घुमा-फिरा के आँच देना, आटे से घेर बाँध के घण्टों गरमाये रखना, ये सब उन्हीं के बस की बात थी। अब्बा के गुजर जाने के बाद तो हम लोग अम्मी को और भी उलझाये रखते कि वे नाहक उनकी याद में जी छोटा न किये रहें। मेरी बीवी तो आप जानिए, जरा भी दखल-अन्दाजी न करती। यूँ भी बेहद खुशमिजाज है, बस पान खाना हँसते रहना।’’ इस बार अनवर गुदगुदाया-सा हँस दिया।
‘‘सच में, अम्मी को कोई टोकनेवाला न था। अम्मी तो तिराहे पर से रसद तक उठवा लातीं। हमारी तो परदें में रहतीं। बस, यूँही, तिराहे-चौराहे पे मुलाकात हो गयी होगी उस शख्स से। बखिया उधेड़ के रख दी हमारी।
खैर ! अम्मी आयें तो भेज दीजिएगा। कहिएगा, उनकी बहुएँ भी तो अब कहाँ इतनी कड़ियल-जवान रह गयी हैं। आखिर औरत को औरत का ही सहारा होता है। तो बीबी, अब इजाजत दें। सलाम।’’
‘‘सलाम !’’–मैं उस शख्स की लौटती पीठ ताकती रह गयी जो बानो का पेट-जाया था, अपना था, सगा था।
अन्धे मोड़
‘‘तुम तो सर-आ-पा गजल हो।’’
अमूल्य ने कहा तो उजाला चौंक गयी। मालूम तो है ही उसे, उजाला की उर्दू-नशीनी। सखुन-शनासी की कायल जानो-तबीयत राजुल ने तो और भी उसकी जानकारी में इजाफा कर दिया होगा। हर किसी से जिक्र कर बैठती है। तब ही तो, उसके जीजाजी ने यह मैरून डायरी हथिया ली थी वही, उजाला का शेर-शायरी का खजाना। मार तमाम, मयखाना-पैमाना से लबरेज थी।
हाशिये पर छरहरी-नाजुक सुराहियाँ अंकित थीं। अगल-बगल अंगूरों के गुच्छे और छलकते जाम। पतली अँगुलियोंवाली जनाना साकी और उसका मेहराबदार माथा। इस सब साजो-सामाँ के बीच खुशकत अशार। उधार के ही सही, वे उजाला की शख्सियत का हिस्सा बन चुके थे।
छलक, हाँ छलक ऐ सागरे हस्ती छलकता रह
यहाँ तक मौत भी आये तो बादाखार हो जाए।
- उसकी सहेली शबनम का खुद का कहा शेर था।
असल शराब की बदजायका बदबू का न शबनम को कोई तजुर्बा था, न उजाला को कोई इल्म। दोनों का मन-मिजाज ऐसा कि बिन पिये ही झूम लें।
‘‘उजाला तो उल्लू के कोटर में भी बुलबुली समाँ बाँध देती है। अमूल्य भला किस मरघट का प्रेत है जो उजाला से मुतासिर न हो ?’’ राजुल का कहना था। उसी राजुल के फूहड़ जीजाजी ने उजाला की गहरे मैरून कवरवाली डायरी की धज्जियों पर धज्जियाँ उड़ा दी थीं। यों चिन्दी-चिन्दी कर हवाओं में बखेर दी थीं, जैसे वह कोई अबाबील का टूटा हुआ घोंसला हो।
राजुल जो उजाला के शायराना अन्दाज पर दरदम सौ जानों से कुर्बानी रहती, कहा करती–
‘‘अगर मैं कोई अमीर-उमरा होती, तो तेरी एक-एक बात पर तुझे जागीर बख्श देती, हाथीखाना और हाथी समेत।’’
जीजाजी की इस जंगली हरकत पर कँपकँपाने लगी।
वह शख्स एक अजीबोगरीब दौरे की गिरफ्त में आ जाता है। पटक-पछाड़ वाली वहशत।
डायरी का चिन्दी-चिन्दी कर देना, महज तैयारी थी। असल अदाकारी तो बाद में आनी थी।
उज्र राजुल ने किया था और पाँचा जड़ा गया, जीजी के गालों पर। पाँच लाल धारियों से जीजी का गाल सनसनाने लगा था।
काश राजुल कोई अरना भैंसा होती तो जीजाजी को उठाके ऐसी पटकनी देती कि कम-अज-कम पाँच पसलियाँ तो चटख-चूर हो रहतीं।
‘‘क्या जानती है तुम्हारी सहेली...वह....वह उजाला, नशेखोरी की बाबत ?’’
वह यों किचकिचाये, मानो अपनी दो-चार दाढ़ों को पीस डालेंगे।
‘‘घटिया और रूमानी सा नजरिया है यह....यूँ डायरी के पन्ने लीप-पोत के शराब पर शायरी, सजा-बनाकर टीप देना। उसने देखा भी है किसी पियक्कड़ को लगा के लड़खड़ाते हुए ? ‘पी के मयखाने से जो रिन्द निकले’.....। जीजाजी ने मुँह टेढ़ा करके जाने कैसे बिचकाया कि लगा उनके ही मुँह से बदबू के भभके उठ रहे हैं। आँखें कपाल तक चढ़कर अघोरी के जैसे हो गयीं। जीजाजी कभी भूले-बिसरे भी दावत-अदावत, खुशी या रंज में कभी घूँट, दो घूँट भी न पीते। यह राजुल का देखा-जाना था और इस सच पर जीजाजी की भी मोहर लगी हुई थी।’’ आखिर राजुल चीख पड़ी, ‘‘जीजाजी ! आपको किसी गैर की डायरी फाड़ देने का कोई इख्तियार नहीं था। मैं अब उजाला को क्या जवाब दूँगी।
अमूल्य ने कहा तो उजाला चौंक गयी। मालूम तो है ही उसे, उजाला की उर्दू-नशीनी। सखुन-शनासी की कायल जानो-तबीयत राजुल ने तो और भी उसकी जानकारी में इजाफा कर दिया होगा। हर किसी से जिक्र कर बैठती है। तब ही तो, उसके जीजाजी ने यह मैरून डायरी हथिया ली थी वही, उजाला का शेर-शायरी का खजाना। मार तमाम, मयखाना-पैमाना से लबरेज थी।
हाशिये पर छरहरी-नाजुक सुराहियाँ अंकित थीं। अगल-बगल अंगूरों के गुच्छे और छलकते जाम। पतली अँगुलियोंवाली जनाना साकी और उसका मेहराबदार माथा। इस सब साजो-सामाँ के बीच खुशकत अशार। उधार के ही सही, वे उजाला की शख्सियत का हिस्सा बन चुके थे।
छलक, हाँ छलक ऐ सागरे हस्ती छलकता रह
यहाँ तक मौत भी आये तो बादाखार हो जाए।
- उसकी सहेली शबनम का खुद का कहा शेर था।
असल शराब की बदजायका बदबू का न शबनम को कोई तजुर्बा था, न उजाला को कोई इल्म। दोनों का मन-मिजाज ऐसा कि बिन पिये ही झूम लें।
‘‘उजाला तो उल्लू के कोटर में भी बुलबुली समाँ बाँध देती है। अमूल्य भला किस मरघट का प्रेत है जो उजाला से मुतासिर न हो ?’’ राजुल का कहना था। उसी राजुल के फूहड़ जीजाजी ने उजाला की गहरे मैरून कवरवाली डायरी की धज्जियों पर धज्जियाँ उड़ा दी थीं। यों चिन्दी-चिन्दी कर हवाओं में बखेर दी थीं, जैसे वह कोई अबाबील का टूटा हुआ घोंसला हो।
राजुल जो उजाला के शायराना अन्दाज पर दरदम सौ जानों से कुर्बानी रहती, कहा करती–
‘‘अगर मैं कोई अमीर-उमरा होती, तो तेरी एक-एक बात पर तुझे जागीर बख्श देती, हाथीखाना और हाथी समेत।’’
जीजाजी की इस जंगली हरकत पर कँपकँपाने लगी।
वह शख्स एक अजीबोगरीब दौरे की गिरफ्त में आ जाता है। पटक-पछाड़ वाली वहशत।
डायरी का चिन्दी-चिन्दी कर देना, महज तैयारी थी। असल अदाकारी तो बाद में आनी थी।
उज्र राजुल ने किया था और पाँचा जड़ा गया, जीजी के गालों पर। पाँच लाल धारियों से जीजी का गाल सनसनाने लगा था।
काश राजुल कोई अरना भैंसा होती तो जीजाजी को उठाके ऐसी पटकनी देती कि कम-अज-कम पाँच पसलियाँ तो चटख-चूर हो रहतीं।
‘‘क्या जानती है तुम्हारी सहेली...वह....वह उजाला, नशेखोरी की बाबत ?’’
वह यों किचकिचाये, मानो अपनी दो-चार दाढ़ों को पीस डालेंगे।
‘‘घटिया और रूमानी सा नजरिया है यह....यूँ डायरी के पन्ने लीप-पोत के शराब पर शायरी, सजा-बनाकर टीप देना। उसने देखा भी है किसी पियक्कड़ को लगा के लड़खड़ाते हुए ? ‘पी के मयखाने से जो रिन्द निकले’.....। जीजाजी ने मुँह टेढ़ा करके जाने कैसे बिचकाया कि लगा उनके ही मुँह से बदबू के भभके उठ रहे हैं। आँखें कपाल तक चढ़कर अघोरी के जैसे हो गयीं। जीजाजी कभी भूले-बिसरे भी दावत-अदावत, खुशी या रंज में कभी घूँट, दो घूँट भी न पीते। यह राजुल का देखा-जाना था और इस सच पर जीजाजी की भी मोहर लगी हुई थी।’’ आखिर राजुल चीख पड़ी, ‘‘जीजाजी ! आपको किसी गैर की डायरी फाड़ देने का कोई इख्तियार नहीं था। मैं अब उजाला को क्या जवाब दूँगी।
’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book