|
जीवन कथाएँ >> सुनहु तात यह अकथ कहानी सुनहु तात यह अकथ कहानीशिवानी
|
156 पाठक हैं |
||||||
शिवानी की जिन्दगी पर आधारित संस्मरण...
चार
एक अद्भुत नारी से कभी मेरा परिचय अल्मोड़ा में ही हुआ था। वह विचित्र मर्दानी वैष्णवी, जो सहसा हमारे घर में धूमकेतु-सी ही प्रकट हुई और उसी धूमकेतु की भाँति विलीन हो गई थी, हमेशा मुझे याद रहेगी। उस दिन हम दोनों बहनें घर में अकेली थीं, 'जय गुरु गोरखनाथ' कह वह अपना डेढ़ गजी चिमटा गाड़ हमारे आँगन में लगे बाग में जम गई।
'माई आज यहीं भोजन पाएगा। उसने कहा और अपनी मोटी-मोटी टाँगें फैला दीं। इतने वर्षों में भी मैं उस भयावह चेहरे को नहीं भूल पाई हूँ। वह पुरुष थी, या नारी? उसके विशाल स्कन्ध, मन्दिर के ताम्रकलश-सा चमकता भस्मपुता ललाट और उग्रतेजी दृष्टि को देखते ही हम दोनों सहम गई थीं लगता था, आँखें नहीं, दो ज्वलन्त अंगारे ही धपधप कर सुलग रहे हैं। सपाट वक्षस्थल में असंख्य रुद्राक्ष स्फटिक की मालाएँ झूल रही थीं और बीचों-बीच एक काले धागे में बँधी एक बड़ी-सी हड्डी खनकती जा रही थी। नहीं यह स्त्री नहीं हो सकती। सहसा उसने अपना गैरिक अधोवस्त्र पुरुषोचित मुद्रा में ऊपर तक उठा अपनी कदली स्तम्भ-सी पुष्ट जाँघों पर चौताल का-सा ठेका बजाया-
जय गुरु, जय-जय गुरु!
जय-जय गुरु, हे, जय गुरु!
वह बोलने में भी पुल्लिंग का प्रयोग कर रही थी, 'जाओ री छोकरियो, अपनी माँ से बेसन, दही, चावल, बर्तन, लकड़ी सब कुछ माँग कर लाओ। माई आज कढ़ी-भात खाएगा...।'
पर माँ थी ही कहाँ? घर में हम दोनों के सिवा कोई भी तो नहीं था।
'जाती क्यों नहीं?' वह गरजी। उसके पृथुल अधरों के ऊपर मूंछों की स्पष्ट रेखा देख हम काँप उठे। यह निश्चय ही कोई प्रवंचक पुरुष हमें अकेली ...। जान हमारा अनिष्ट करने ही आ धमका है। शायद हमारे संशय को मिटाने के लिए ही अचानक उसने फिर बड़ी बेशर्मी से अपना गैरिक उत्तरीय-सलूका उतार पत्थर पर रख दिया। सूखी तूंबी से लटके फिर उसके नारीत्व के स्पष्ट प्रमाण-पत्र ने हमारी आशंका स्वयं दूर कर दी। वह औरत ही थी, सौ फीसदी औरत।
उसी वर्ष अल्मोड़ा को एक खबर ने हिला कर रख दिया था। अल्मोड़ा में सहसा महामारी-सी एक भैरवी आ धमकी थी। हम अनेक कहानियाँ उसके बारे में सन भी चुके थे। कहते थे, जहाँ वह चिमटा गाड़ कर जम जाती, उस गृहस्वामी का या तो शतमुखी सर्वनाश कर जाती, या फिर उसे मालामाल कर देती। किसी का इकलौता पुत्र देखते ही देखते आँखें पलट देता, तो किसी की पत्नी निर्वस्त्र सड़कों पर भागने लगती।
कहीं यह उसी अखाड़े की कोई भैरवी तो नहीं थी, या स्वयं वही? पर जो भी थी, हम उसकी आँखों से आँखें मिला कर बात नहीं कर पा रहे थे। हमने सब चीजें लाकर रख दीं। उसने कढ़ी-भात भी बनाया, हमें भी प्रसाद दिया। फिर वह अर्धोन्मीलित दृष्टि से हमें देखती सहसा बहुत दूर चली गई। हम बर्तन धोकर भीतर रखने गए, जब लौटे, तो देखा, वह समाधिस्थ हो मूर्तियत् पद्मासन लगा कर अडिग बैठी है।
कुछ घंटों ही पूर्व, जिसकी मर्दानी सूरत देख हम सहम गए थे, उसी चेहरे पर जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी फेर दी थी। दिव्य दमकता तेजस्वी चेहरा। दगदगाते ललाट से जैसे चन्द्रमा की शीतल किरणें झरझरा कर बह रही थीं। कहाँ विलीन हो गईं वे अस्वाभाविक मूंछे और दाँत? न जाने कौन-सी शक्ति, हमें चुम्बक-सा खींचती उनके चरणों पर गिरा गई। उन्होंने हमारा माथा छुआ। कैसा अद्भुत था वह ज्योतिर्मय स्पर्श! लगता था शरीर का एक-एक शिरा झनझना उठा है। अपने गैरिक उत्तरीय से उन्होंने अपना माथा ढाँक लिया था। 'वासं वासना तरुणार्क राग।'
फिर हँस कर बोली, “पूछ, कुछ पूछना है?" हमारी कुछ बचकानी शंकाओं का उत्तर दे वह एक झटके से खड़ी हो गईं।
'जय गुरु गोरखनाथ' ! कह कर चिमटा उखाड़ा और पोटली थामे, बिना पीछे मुड़े आँधी-सी ओझल हो गईं। सुना था कि साधु-सन्त कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखते, अब प्रत्यक्ष देख भी लिया।
निश्चय ही, वह कोई सिद्ध योगिनी थीं। जाने लगी, तो मैंने ही हाथ पकड़ कर उन्हें उठाया था। उनका वह क्षणिक दिव्य स्पर्श ही शायद मेरे इस तुच्छ हाथ को थोड़ा बहुत लिखने की क्षमता दे गया।
इतने वर्षों बाद भी जब किसी कठिन विपत्ति के दलदल में फँसने लगती हूँ, या किसी की कटुवाणी का आघात, चाबुक-सा मार उठता है, तब उसी वैष्णवी के गिरगिट से बदल गए ललित मोहन रूप का स्मरण करती हूँ, तो लगता है, पलभर में मेरा हाथ पकड़ उन्होंने मुझे दलदल से बाहर खींच लिया है। स्वयं मेरी सत्ता उसी क्षण समाप्त हो जाती है, यह मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, एक नहीं कई बार।
सहसा विधाता ने हमें जन्मभूमि का मोह त्यागने को बाध्य कर सुदूर सौराष्ट्र भेज दिया। पिता वहीं राजकुमार कॉलेज में भारत की विभिन्न रियासतों के राजपुत्रों के शिक्षक थे-दतिया, जूनागढ़, रामपुर, माणावदर, जसदण, राजकोट, मायसोर आदि प्रतिष्ठित रियासतों के राजकुमार मेरे पिता के शिष्य बने। तब राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल थे विख्यात शिक्षाविद् मि. टर्नर। कभी-कभी मुझे अपनी स्मरण-शक्ति पर गर्व होता है कि तब मैं कितनी छोटी रही होऊँगी, किन्तु मुझे आज भी वे सब चेहरे एकदम सही-सही याद हैं-राजकोट के ठाकुर साहब, जसदण के युवराज आला खाचर, जीवा खाचर, कमला बा, उनकी पुत्री लीला बा, माधवी देवी, रामपुर के वली अहद, यहाँ तक कि नागर ब्राह्मणों की हवेली से सटा हमारा घर, वह बड़ा-सा हॉल, जहाँ पीतल के चमचमाते पिंजरे में बन्दी अफ्रीका का बहुरंगी काकातुआ निरन्तर एक ही रट लगाता रहता'केम छो? राम-राम केम छो?' पड़ोस के कोकिल भाई, रसिक भाई, हरिच्छा बेन, उर्मिला बेन और रौबदार गृहस्वामिनी मासी बा।
मैं तब छोटी थी, इसी से स्कूल में प्रवेश नहीं मिला, पर अपनी बड़ी बहन जयन्ती को स्कूल पहुँचाने मैं अवश्य जाती। दोमंजिला मिशन स्कूल की ऊँची इमारत शायद अब भी वैसी ही हो, तब वह राजकोट का एकमात्र कन्या विद्यालय था। बड़ी बहन मुझे स्कूल पहुंचते ही बाहर से विदा कर देती। मैं ललचाई दृष्टि से देखती कि जयन्ती अपनी सखियों से बतियाती-किलकती जा रही है-बदरुन्निसा, रेचल, ऐस्थर।
हमारा परिवार पूरे चौदह वर्ष तक राजकोट में रहा, फिर जैसे-जैसे पिता के युवराज शिष्यों को गद्दी मिली, वे उन्हें बड़े आदर से बुलाते रहे-माणावदर, बीरावल, कभी जूनागढ़, कभी अलीराजपुर। सुदीर्घ सौराष्ट्र प्रवास ने हमें गुजराती ही बना दिया। यद्यपि नौकर, रसोइया, सब पहाड़ी थे, पर खाना सौ फीसदी गुजराती बनता। समय भी वही अर्थात् सूर्यास्त से पूर्व रात्रि का भोजन। वह नियम वर्षों तक कायम रहा, फिर पुत्रों के विवाह हुए। बहुएँ आईं, तो अलबत्ता उन्हें यह विचित्र लंच-डिनर टाइमिंग रास नहीं आई, “यह भी कोई वक्त है खाने का? यह तो शाम की चाय का वक्त है जी।" खैर, वह अलग कहानी है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book









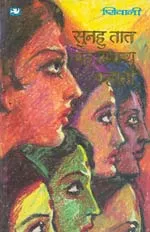


_s.webp)
