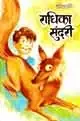|
नारी विमर्श >> चौदह फेरे (सजिल्द) चौदह फेरे (सजिल्द)शिवानी
|
99 पाठक हैं |
||||||
चौदह फेरे लेनेवाली कर्नल पिता की पुत्री अहल्या जन्म लेती है अल्मोड़े में, शिक्षा पाती है ऊटी के कान्वेन्ट में, और रहती है पिता की मुँहलगी मल्लिका की छाया में। और एक दिन निर्वासित, हिमालय में तपस्यारत माता के प्रबल संस्कारों से बँध सहसा ही विवाह के दो दिन पूर्व वह भाग जाती है,
CHAUDAH PHERE
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
चौदह फेरे लेनेवाली कर्नल पिता की पुत्री अहल्या जन्म लेती है अल्मोड़े में, शिक्षा पाती है ऊटी के कान्वेन्ट में, और रहती है पिता की मुँहलगी मल्लिका की छाया में। और एक दिन निर्वासित, हिमालय में तपस्यारत माता के प्रबल संस्कारों से बँध सहसा ही विवाह के दो दिन पूर्व वह भाग जाती है, कुमाऊँ अंचल में।
समूचा उपन्यास विविध प्राणवान् चरित्रों, समाज, स्थान तथा परिस्थितियों के बदलते हुए जीवन मूल्यों के बीच से गुजरता है।
आदि से अन्त तक भरपूर रोचक तथा अविस्मरणीय।
समूचा उपन्यास विविध प्राणवान् चरित्रों, समाज, स्थान तथा परिस्थितियों के बदलते हुए जीवन मूल्यों के बीच से गुजरता है।
आदि से अन्त तक भरपूर रोचक तथा अविस्मरणीय।
शिवानी
यों तो एक कहानी लेखिका के रूप में शिवानी ने कई वर्ष पहले मेरा ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन मुझे बराबर यह अनुभव होता था कि उन्हें आगे चल कर उपन्यास लिखने चाहिए। कहानियों में जिस तरह से सजीव चित्रण के उभारती थीं, उनकी सही जगह उपन्यासों में थी, ऐसा मेरा विश्वास था। उनकी हर कहानी एक विशेष मोड़ तक जाकर रुक जातीं थी और मैं सोचा करता था कि इसके आगे भी बहुत-कुछ होना चाहिए।
इसलिए जब ‘धर्मयुग’ में ‘चौदह फेरे’ धारावाहिक छपने लगा तो मुझे एक आन्तरिक प्रसन्नता हुई, केवल इसलिए नहीं कि मेरा सोचा हुआ सम्भव हुआ बल्कि इसलिए भी कि मुझे एक अच्छा उपन्यास पढ़ने के लिए मिलने लगा। धारावाहिक छपनेवाले उपन्यास पढ़ने में मुझे बड़ी उलझन होती है। एक बैठक में पुस्तक खत्म कर देने की मेरी पुरानी आदत बीच में ही टूट जानेवाली धारावाहिक की धारा से सन्तुष्ट नहीं होती। इसलिए ऐसे उपन्यास पढ़ने का मैं प्रयत्न ही नहीं करता। लेकिन ‘चौदह फेरे’ के साथ मैं ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद भी उनके कई उपन्यास धारावाहिक छपने तक मेरे भीतर का रस-स्त्रोत ही छीज गया हो लेकिन मेरे मन में अब भी यह बात जमी हुई है कि शिवानी के ‘चौदह फेरे’ में दूध-जैसी ताज़गी थी, वह बाद के उपन्याओं की प्रौढ़ता और चिन्तन के चलते कुछ उपेक्षित-सी हो गयी। इसके मतलब यह भी नहीं है कि समय के चलते लेखक में आनेवाले प्रौढ़ता कोई अनावश्यक तत्त्व है। शिवानी ने इधर अपना लेखनीय व्यक्तित्व विकसित किया है और सौभाग्य से उन्हें अपने समकालीन लेखकों की तुलना में कहीं अधिक पाठक मिले हैं।
वे एक सफल लेखिका हैं और उनकी रचनाओं की ओर पाठकों की दृष्टि लगी रहती है। मैंने अभी-अभी उनकी लगभग सभी रचनाएँ एक बार फिर पढ़ी और मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वे अपने ऊपर चारों ओर से पड़ रहे प्रकाश-बिम्बों से एक हद तक विचलित पर काफी हद तक सजग है। लेखक के जीवन में ऐसे क्षण बहुत महत्त्वपूर्ण होते है जब उसकी रचना सही माने में प्रकाश में आती है। यह एक प्रसन्नता की घड़ी होती है लेकिन प्रसन्नता का आवेग शीघ्र ही एक अदृश्य आशंका का स्थान ले लेता है और लेखक धीरे-धीरे स्वयं के प्रति सजग होने लगते है। यह सजगता कभी-कभी लेखक के भीतर की अजान परतें तोड़ती है और उसे अनथाही गहराइयों की ओर जाने को बाध्य करती है। लेखक के लिए यह एक अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ऐसा भी हुआ है कि प्रसिद्ध और प्रशंसा लेखक को विजड़ित या स्तम्भित कर देती हैं। ‘चौदह फेरे’ के प्रकाशन के बाद के वर्षों में शिवानी ने जो कुछ लिखा है, वह एक लेखक के इसी दुरूह संघर्ष का प्रतिफल है।
‘चौदह फेरे’ के कथानक की उन्मुक्त सादगी और कौशल की पहाड़ी चित्रकला-जैसी चटख रंगीन अब भी शिवानी की सबसे बड़ी शक्ति है। अपने नवीनतम उपन्यास ‘भैरवी’ तक में उन्होंने वातावरण बनाने और रूप-चित्रण करने में अपनी ‘चौदह फेरे’ की कारीगरी सुरक्षित रखी; लेकिन आलोचकों ने इसी बीच उनकी इसी कुशलता पर उँगली उठानी शुरू कर दी है। ये इसे दुहराव कहते हैं और लेखिका की सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं। मैं आलोचकों के मत के विरुद्ध या पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन उनसे इतना अवश्य पूछूँगा कि वे लेखकों की भीड़ में से एक विशेष-लेखन को अलग से किस तरह पहचानते हैं। वे शायद शैली की विशिष्टता की बात कहें या इससे मिलती-जुलती और कुछ बातें, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का उत्तर देते-देते शिवानी पर लगाये गये अपने आरोपों का खण्डन वे अपने-आप ही कर देंगे। सम्पूर्ण संस्कृति वाड़्मय में बाणभट्ट की कादम्बरी का छोटे-से-छोटा अंश भी अलग से पहचाना जा सकता है, वैसे ही जैसे आप हिन्दी गद्य लेखकों की भीड़ में श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी या उनके स्तर के शैलीकारों को अलग से पहचान लेते है। शिवानी के सम्बन्ध में भी यह बात बिना हिचक के कही जा सकती है।
शिवानी की रचनाएँ पाठकों द्वारा प्रशंसित होने पर भी हिन्दी के लेखकों तथा आलोचकों द्वारा लगभग उपेक्षित ही रही है। यहाँ एक ऐसा तथ्य है जिसे शिवानीजी के सन्दर्भ में नज़रअन्दाज कर भी दिया जाए लेकिन साहित्य की संप्रेषणीयता के सन्दर्भ में इसकी पाठक के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए स्पष्ट रूप से संप्रेषणीयता के प्रश्न पर दो पक्ष हो गये है। नये लेखकों की एक बड़ी संख्या अपनी रचना पर संप्रेषणीयता का कोई दबाव अनुभव नहीं करती या करना नहीं चाहती। बहुत-सारी प्रतिबद्धताओं और प्रतिष्ठानों के विरुद्घ खड़े होने की घोषणा करने वाले लेखक उसी झटके में रचना के संप्रषणीय होने के एक महत्त्वपूर्ण गुण के विरुद्ध भी ख़ड़े हो गये हैं। दूसरा पक्ष संप्रेषणीयता को एक आवश्यक गुण मानता है। यों तो इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के पास तर्क हैं और इस पर देर तक बातें भी का जा सकती है लेकिन यहाँ इस प्रश्न को उठाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि भविष्य में जब लोग इस प्रश्न पर विचार करें तो वे शिवानी-जैसी लोकप्रिय लेकिन आलोचको द्वारा लगभग उपेक्षित लेखिका के रचना-धर्म पर भी एक बार अवश्य सोचने पर बाध्य हों।
शिवानी उन कुछ उपन्यासकारों की कोटि की लेखिका नहीं है जिन्हें आलोचक आसानी से उड़ा दिया करते हैं। यहाँ उन तथाकथित उपन्यासकारों के बारें में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वे समृद्ध कथानक और जीवन्त परिवेश की लेखिका है तथा उन्होंने विविधतापूर्ण और संस्कारयुक्त जीवन जिया है। वे चाहें भी तो अपनी इस पूरे जीवन की कमाई से अपने को अलग नहीं कर सकतीं। इसलिए जब आलोचक उनके इन गुणों को दोष बना देते हैं तो लगता है कि जैसे उनसे कहीं कोई गलती हो रही है। हिन्दी एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा है और उसमें विभिन्न स्तरों के लेखक लिखने के लिए एक-जैसी भाषा बोलें और एक जैसी परिस्थियों में जियें, यह सम्भव नहीं यदि ऐसा होता तो हिन्दी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं होगा। पश्चिमी देशों के बड़े नगरों की कुढ़न को व्यक्त करने वाली भाषा हिन्दुस्तान ऐसे पूरे देश की भाषा नहीं बन सकेगी, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मेरा यह विश्वास जिन कुछ लेखकों के बल पर दृढ़ होता है, उनमें शिवानी भी हैं। साहित्य और साहित्य जो काल्पनिक भेद बना लिये है वे आज नहीं तो कल टूटेगे। शिवानी एक लोकप्रिय लेखिका है और तथाकथित श्रेष्ठ सहित्य के चौखटों में न जड़ी जाकर भी वे बहुत घाटे में नहीं रहेगीं। मुझे विश्वास है कि वे अपने भीतर के रचनाकार के प्रति और अधिक सजगता बरतेंगी और भविष्य में इस बात के लिए कभी उदास नहीं होंगी कि उन्हें उन कुछ लोगों ने याद नहीं किया जो मात्र कुछ लोग ही थे।
इसलिए जब ‘धर्मयुग’ में ‘चौदह फेरे’ धारावाहिक छपने लगा तो मुझे एक आन्तरिक प्रसन्नता हुई, केवल इसलिए नहीं कि मेरा सोचा हुआ सम्भव हुआ बल्कि इसलिए भी कि मुझे एक अच्छा उपन्यास पढ़ने के लिए मिलने लगा। धारावाहिक छपनेवाले उपन्यास पढ़ने में मुझे बड़ी उलझन होती है। एक बैठक में पुस्तक खत्म कर देने की मेरी पुरानी आदत बीच में ही टूट जानेवाली धारावाहिक की धारा से सन्तुष्ट नहीं होती। इसलिए ऐसे उपन्यास पढ़ने का मैं प्रयत्न ही नहीं करता। लेकिन ‘चौदह फेरे’ के साथ मैं ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद भी उनके कई उपन्यास धारावाहिक छपने तक मेरे भीतर का रस-स्त्रोत ही छीज गया हो लेकिन मेरे मन में अब भी यह बात जमी हुई है कि शिवानी के ‘चौदह फेरे’ में दूध-जैसी ताज़गी थी, वह बाद के उपन्याओं की प्रौढ़ता और चिन्तन के चलते कुछ उपेक्षित-सी हो गयी। इसके मतलब यह भी नहीं है कि समय के चलते लेखक में आनेवाले प्रौढ़ता कोई अनावश्यक तत्त्व है। शिवानी ने इधर अपना लेखनीय व्यक्तित्व विकसित किया है और सौभाग्य से उन्हें अपने समकालीन लेखकों की तुलना में कहीं अधिक पाठक मिले हैं।
वे एक सफल लेखिका हैं और उनकी रचनाओं की ओर पाठकों की दृष्टि लगी रहती है। मैंने अभी-अभी उनकी लगभग सभी रचनाएँ एक बार फिर पढ़ी और मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वे अपने ऊपर चारों ओर से पड़ रहे प्रकाश-बिम्बों से एक हद तक विचलित पर काफी हद तक सजग है। लेखक के जीवन में ऐसे क्षण बहुत महत्त्वपूर्ण होते है जब उसकी रचना सही माने में प्रकाश में आती है। यह एक प्रसन्नता की घड़ी होती है लेकिन प्रसन्नता का आवेग शीघ्र ही एक अदृश्य आशंका का स्थान ले लेता है और लेखक धीरे-धीरे स्वयं के प्रति सजग होने लगते है। यह सजगता कभी-कभी लेखक के भीतर की अजान परतें तोड़ती है और उसे अनथाही गहराइयों की ओर जाने को बाध्य करती है। लेखक के लिए यह एक अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ऐसा भी हुआ है कि प्रसिद्ध और प्रशंसा लेखक को विजड़ित या स्तम्भित कर देती हैं। ‘चौदह फेरे’ के प्रकाशन के बाद के वर्षों में शिवानी ने जो कुछ लिखा है, वह एक लेखक के इसी दुरूह संघर्ष का प्रतिफल है।
‘चौदह फेरे’ के कथानक की उन्मुक्त सादगी और कौशल की पहाड़ी चित्रकला-जैसी चटख रंगीन अब भी शिवानी की सबसे बड़ी शक्ति है। अपने नवीनतम उपन्यास ‘भैरवी’ तक में उन्होंने वातावरण बनाने और रूप-चित्रण करने में अपनी ‘चौदह फेरे’ की कारीगरी सुरक्षित रखी; लेकिन आलोचकों ने इसी बीच उनकी इसी कुशलता पर उँगली उठानी शुरू कर दी है। ये इसे दुहराव कहते हैं और लेखिका की सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं। मैं आलोचकों के मत के विरुद्ध या पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन उनसे इतना अवश्य पूछूँगा कि वे लेखकों की भीड़ में से एक विशेष-लेखन को अलग से किस तरह पहचानते हैं। वे शायद शैली की विशिष्टता की बात कहें या इससे मिलती-जुलती और कुछ बातें, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का उत्तर देते-देते शिवानी पर लगाये गये अपने आरोपों का खण्डन वे अपने-आप ही कर देंगे। सम्पूर्ण संस्कृति वाड़्मय में बाणभट्ट की कादम्बरी का छोटे-से-छोटा अंश भी अलग से पहचाना जा सकता है, वैसे ही जैसे आप हिन्दी गद्य लेखकों की भीड़ में श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी या उनके स्तर के शैलीकारों को अलग से पहचान लेते है। शिवानी के सम्बन्ध में भी यह बात बिना हिचक के कही जा सकती है।
शिवानी की रचनाएँ पाठकों द्वारा प्रशंसित होने पर भी हिन्दी के लेखकों तथा आलोचकों द्वारा लगभग उपेक्षित ही रही है। यहाँ एक ऐसा तथ्य है जिसे शिवानीजी के सन्दर्भ में नज़रअन्दाज कर भी दिया जाए लेकिन साहित्य की संप्रेषणीयता के सन्दर्भ में इसकी पाठक के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए स्पष्ट रूप से संप्रेषणीयता के प्रश्न पर दो पक्ष हो गये है। नये लेखकों की एक बड़ी संख्या अपनी रचना पर संप्रेषणीयता का कोई दबाव अनुभव नहीं करती या करना नहीं चाहती। बहुत-सारी प्रतिबद्धताओं और प्रतिष्ठानों के विरुद्घ खड़े होने की घोषणा करने वाले लेखक उसी झटके में रचना के संप्रषणीय होने के एक महत्त्वपूर्ण गुण के विरुद्ध भी ख़ड़े हो गये हैं। दूसरा पक्ष संप्रेषणीयता को एक आवश्यक गुण मानता है। यों तो इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के पास तर्क हैं और इस पर देर तक बातें भी का जा सकती है लेकिन यहाँ इस प्रश्न को उठाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि भविष्य में जब लोग इस प्रश्न पर विचार करें तो वे शिवानी-जैसी लोकप्रिय लेकिन आलोचको द्वारा लगभग उपेक्षित लेखिका के रचना-धर्म पर भी एक बार अवश्य सोचने पर बाध्य हों।
शिवानी उन कुछ उपन्यासकारों की कोटि की लेखिका नहीं है जिन्हें आलोचक आसानी से उड़ा दिया करते हैं। यहाँ उन तथाकथित उपन्यासकारों के बारें में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वे समृद्ध कथानक और जीवन्त परिवेश की लेखिका है तथा उन्होंने विविधतापूर्ण और संस्कारयुक्त जीवन जिया है। वे चाहें भी तो अपनी इस पूरे जीवन की कमाई से अपने को अलग नहीं कर सकतीं। इसलिए जब आलोचक उनके इन गुणों को दोष बना देते हैं तो लगता है कि जैसे उनसे कहीं कोई गलती हो रही है। हिन्दी एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा है और उसमें विभिन्न स्तरों के लेखक लिखने के लिए एक-जैसी भाषा बोलें और एक जैसी परिस्थियों में जियें, यह सम्भव नहीं यदि ऐसा होता तो हिन्दी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं होगा। पश्चिमी देशों के बड़े नगरों की कुढ़न को व्यक्त करने वाली भाषा हिन्दुस्तान ऐसे पूरे देश की भाषा नहीं बन सकेगी, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मेरा यह विश्वास जिन कुछ लेखकों के बल पर दृढ़ होता है, उनमें शिवानी भी हैं। साहित्य और साहित्य जो काल्पनिक भेद बना लिये है वे आज नहीं तो कल टूटेगे। शिवानी एक लोकप्रिय लेखिका है और तथाकथित श्रेष्ठ सहित्य के चौखटों में न जड़ी जाकर भी वे बहुत घाटे में नहीं रहेगीं। मुझे विश्वास है कि वे अपने भीतर के रचनाकार के प्रति और अधिक सजगता बरतेंगी और भविष्य में इस बात के लिए कभी उदास नहीं होंगी कि उन्हें उन कुछ लोगों ने याद नहीं किया जो मात्र कुछ लोग ही थे।
1.दिसम्बर, 1970
लखनऊ
लखनऊ
-ठाकुरप्रसाद सिंह
कुमाऊँ से मेरा सम्बन्ध, सदा के उस भाग्यहीन सन्तान का-सा रहा, जो जन्मते ही माँ से बिछुड़ जाती है। मेरा जन्म हुआ स्वदेश से दूर, सौराष्ट्र के राजकोट नगर में। घर में गुजराती बोली जाती थी, बोल फूटते ही हमने माँ को ‘बा’ कहना सीखा। पहाड़ी सर-भात का स्थान गुजराती खटमिट्ठी को कम डली दाल ने ले लिया था। पहाड़ से साथ आये पहाड़ी नौकर भी अपनी मातृभाषा भूलने लगे थे। राजकोट की मुझे अभी भी खूब याद है। हमारे सामने ही नागर ब्राह्मणों की ऊँची हवेली की खिड़की हमारी खिड़की से सटी-सटी थी। वहीं से गुजरती गाठिया और ‘गोड़केरी नूँ अथाणूं’ (आम की मीठी अचारी) के साथ पहाड़ी अखरोटों का ‘बार्टर प्रणाली’ से अदान-प्रदान चलता रहता। रसिक भाई, कोकिल भाई, उर्मिला बेन और हरिच्छा बेन के गोल-लम्बे चेहरे अभी भी स्मृतिपलट धुँधले पेन्सिलस्केच-से उभर आते हैं।
बीच-बीच में बड़ी-सी मोटर में बैठकर हम पिताजी के छात्र, जसदन के बापा साहब के महल में जाते तो माधवी रानी बड़े प्रेम से अपनी पुत्री लीला बा के साथ खेलने के लिए मुझे रोक लेतीं। रात-भर उनके विराट महल की जहाज-सी पलंग में उठ-उठकर बैठ जाती और घर, माँ के पास जाने के लिए रोती रहती। सुबह उठते ही महल के लम्ब-तंडग भूत-से अरबी-नौकरों को देखकर सहम कर रह जाती, थोड़ी देर में ‘खम्मा’ ‘खम्मा’ करती दासियों की रंगीन फौज हमें बाग में घुमाने ले जाती, हिचके में पेंग दे-देकर झुलाती और मैं घर के लिए रोना भूल जाती। पहाड़ जाना सात-आठ वर्ष तक हो नहीं पाया। मेरे पिताजी राजकुमार कॉलेज़ में कई राजकुमारों के गार्जियन ट्यूटर थे। उन दिनों राजकुमार कॉलेज अपने ढंग की अनोखी संस्था मानी जाती थी।, मेरे पिताजी अपनी विदेश की शिक्षा; रोबीले व्यक्तित्व और कठोर अनुशासन के कारण प्रिन्सवर्ग में बहुत जनप्रिय थे। एक से एक बड़ी रियासतों के राजपूत आग्रह कर, उनके ‘हाउस’ में पढ़ने आते। उन दिनों कुछ राजकुमारों को पब्लिक स्कूल की भाँति एक हाउस-मास्टर के अनुशासन में रहता होता था। मांणावदर, रामपुर, जूनागढ़, मैसूर, जसदन, ओरछा, दलित आदि के अनेक राजकुमार उनके छात्र थे। दतिया के राजकुमार, उन्हें पिताजी प्यार से बुलबुल पुकारते थे, एक लम्बे अर्सें तक हमारे गृह-सदस्य के रूप में मेरी माँ के साथ रहे। एक-एक कर पिताजी के राजसी छात्र, राजा बने और सब ने गुरू का स्मरण किया।
पहले पिताजी मांणावदर के नवाब के यहाँ उच्च पद पर नियुक्त हुए। बिरावल के गरजते-उमड़ते समुद्र के पास हमारा बँगला था, हमारे पुराने महाराज, लोह-नीजी, नित्य नियमपूर्वक आरती के समय हम दोनों भाई-बहनों को सोमनाथ के मन्दिर में ले जाते और उनके साथ-में-स्वर मिलाकर, हम दोनों शिव के उस प्रसिद्ध मन्दिर को देवी-स्तुति से गुँजाते हैः
बीच-बीच में बड़ी-सी मोटर में बैठकर हम पिताजी के छात्र, जसदन के बापा साहब के महल में जाते तो माधवी रानी बड़े प्रेम से अपनी पुत्री लीला बा के साथ खेलने के लिए मुझे रोक लेतीं। रात-भर उनके विराट महल की जहाज-सी पलंग में उठ-उठकर बैठ जाती और घर, माँ के पास जाने के लिए रोती रहती। सुबह उठते ही महल के लम्ब-तंडग भूत-से अरबी-नौकरों को देखकर सहम कर रह जाती, थोड़ी देर में ‘खम्मा’ ‘खम्मा’ करती दासियों की रंगीन फौज हमें बाग में घुमाने ले जाती, हिचके में पेंग दे-देकर झुलाती और मैं घर के लिए रोना भूल जाती। पहाड़ जाना सात-आठ वर्ष तक हो नहीं पाया। मेरे पिताजी राजकुमार कॉलेज़ में कई राजकुमारों के गार्जियन ट्यूटर थे। उन दिनों राजकुमार कॉलेज अपने ढंग की अनोखी संस्था मानी जाती थी।, मेरे पिताजी अपनी विदेश की शिक्षा; रोबीले व्यक्तित्व और कठोर अनुशासन के कारण प्रिन्सवर्ग में बहुत जनप्रिय थे। एक से एक बड़ी रियासतों के राजपूत आग्रह कर, उनके ‘हाउस’ में पढ़ने आते। उन दिनों कुछ राजकुमारों को पब्लिक स्कूल की भाँति एक हाउस-मास्टर के अनुशासन में रहता होता था। मांणावदर, रामपुर, जूनागढ़, मैसूर, जसदन, ओरछा, दलित आदि के अनेक राजकुमार उनके छात्र थे। दतिया के राजकुमार, उन्हें पिताजी प्यार से बुलबुल पुकारते थे, एक लम्बे अर्सें तक हमारे गृह-सदस्य के रूप में मेरी माँ के साथ रहे। एक-एक कर पिताजी के राजसी छात्र, राजा बने और सब ने गुरू का स्मरण किया।
पहले पिताजी मांणावदर के नवाब के यहाँ उच्च पद पर नियुक्त हुए। बिरावल के गरजते-उमड़ते समुद्र के पास हमारा बँगला था, हमारे पुराने महाराज, लोह-नीजी, नित्य नियमपूर्वक आरती के समय हम दोनों भाई-बहनों को सोमनाथ के मन्दिर में ले जाते और उनके साथ-में-स्वर मिलाकर, हम दोनों शिव के उस प्रसिद्ध मन्दिर को देवी-स्तुति से गुँजाते हैः
‘बाघम्बरवाली कर दे दिलों के दुःख दूर
कोई चढ़ावै ध्वाजा पताका
कोई चढ़ावै फूल
जय बाघम्बरवाली।’
कोई चढ़ावै ध्वाजा पताका
कोई चढ़ावै फूल
जय बाघम्बरवाली।’
‘पर कोहनीजी, यह तो देवी की स्तुति है’, मैं कहती।
‘चुप छोकरी’, वे धमक लगाकर फिर झूमने लगते।
‘असल में बूढ़ज्यू को शिव की स्तुति आती नहीं’, मेरा भाई कहता और हम दोनों भाव-विभोर लोहनीजी के साथ बड़ी देर तक आरती गाते रहते। मांणावदर रहने के पश्चात् रामपुर में पिताजी की नियुक्ति हुई गृहमन्त्री के पद पर। मेरे पितामह, काशी विश्वविद्यालय में धर्म-प्रचारक के पद पर थे। वे कुमाऊँ के पहले ग्रेजुएट थे, साथ ही संस्कृति के धुरन्दर विद्धान् और और दबंग वकील। उन्हें पिताजी की इस ऊँची नौकरी के प्रसन्नता नहीं हुई। मालवीयजी की इच्छा नहीं थी कि पिताजी रामपुर जायें, वे मेरे पितामह के अन्तरंग मित्र थे और उनसे सलाह लेकर मेरे पितामह ने पिताजी को राजकोट ही रहने दिया; पर तब तक हम सब रामपुर आ चुके थे।
हम भाई-बहनों की साहबी शिक्षा भी पितामाह के आदर्शों के विपरीत हो रही थी। बड़े-भाई के लिए नैनिताल में एक बँगला ले दिया था, वहीं एक अंग्रेज गवर्नेस मिस स्मिथ से पढ़ने नित्य उनके बँगले में जाना पड़ता था। मि० स्मिथ विलायत से पहली बार भारत आये थे, इसी से पति-पत्नि को हिन्दी एकदम ही नहीं आती थी। कभी-कभी वे दोनों नये शब्द का हिन्दी उल्था लिखने ही में पूरा समय बिता देते। सुबह 6 बजे, मुझे घुड़सवारी सिखाने आते बूढे़ सिकन्दर मियाँ उनके राख के रंग के लहकदार साफे की लम्बी चोटी उनकी चौड़ी पीठ पर भरतनाट्यम की नर्तकी के पंख-सी बड़ी अन्दाज से फैली रहती। उनकी मेंहदी से रँगी दाढ़ी और मूछों के संगम पर, पान के छींटे फुलकारी-सी किये रहते।
‘इन्शाअल्ला, बिट्टो, तुम अब घुड़सवारी में किसुनभैया को भी पछाड़ सकती हो’, वे कहते और मैं गर्व से फूल उठती। किसुनभैया के पिता श्री बृजचन्द्र शर्मा मेरे पिता जी अभिन्न मित्र थे और वहीं रेवेन्यू मिनिस्टर थे। एक दिन कुआँ फाँदने की हर्डल में मैंने सचमुच ही ‘किसुन भैया’ को हरा दिया, तो सिकन्दर मियाँ ने मेरा माथा चूम लिया। तब मैं सचमुच ही उनके बाजी मार ले गयी थी, पर जिन्दगी की दौड़ में घोड़ा भगाते अब मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं। कुछ वर्ष पूर्व पेंकिग में एक उच्च पदस्थ फौजी अफसर थे। अपने फौज़ी बिल्लों के बीच अब तो शायद कई सोने के तमगे लटका चुके होंगे, पर भाग्य की विडम्बना देखिए कि वर्षों पहले उन्हें घुड़सवारी में पछाड़ने पर आज तक मैं एक तमगा भी नहीं जुटा पायी।
हमारे बँगले का नाम था : ‘मुस्तफा लॉज। बँगला क्या, अच्छा-खासा इमामबाड़ा था। लाल ईंटों की बनी वह भव्य कोठी वर्षों से होम साहब की कोठी राही थी। उनके सामने बहुत बड़ा मखमली लॉन था। मेहराबदार ड्योढ़ी में चार-चार सन्तरी, ऊँची संगीनें उठाये दिन-रात सख्त पहरा देते थे। उन दिनों हिन्दू होम साहब की सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध रहता था। बाग में रंगीन क्यारियों में नीले, ऊदे फूलों को घेरे मेंहदी में ऊँची बाड़ को, सरूपा माली दिन-रात तर किये रहता। भींगी मेंहदी की मीठी खुशबू-इश्कपेंचा की बेल पर चढती, पूरे छज्जे पर फैल जाती है; जहाँ तख्त लगाकर मशीन घरघराता मूलचन्द्र दर्जी हमारे लिए चक्की के पाट-सी पायंचो की सलवारें और रामपुर के खास चुन्नट पड़े ढीले कुर्तें सिलता, जिनकी बाँहों में हीना और खस की चुटकियाँ भरने, काने चमन मियाँ अपनी एक आँख के ज्योतिपुंज का जुगनू चमकते सहस्त्र चुन्नटें डालते। आज भी आँखें बन्द करके उस बिसरी सुगन्ध की स्मृति के नथुनों भींचकर सूंघने की चेष्टा करती हूँ, पर कुछ भी हाथ नहीं लगता।
हमारे दीवानखाने में चारों ओर किताबों का अम्बार चुना रहता, घर का पत्येक व्यक्ति पढ़ने के पीछे दीवाना था, यहाँ तक कि बूढ़ें लोहनीजी भी बिना पढ़े नींद नहीं आती थी। हमारी माँ की गुजराती पुस्तकों का भण्डार नित्य नवीन रहता। मुंशी, मेघाणी उनके प्रिय लेखक थे। एक बार छिपाकर ‘सरस्वतीचन्द्र’ पढ़ने पर माँ का जो करारा चाँटा पड़ा था। वह भी नहीं भूलता।
अतिथियों का मेला नित्य लगा ही रहता। पिताजी अपने आतिथ्य और ऊँची पसन्द के ‘सेलर’ के लिए प्रसिद्ध थे। अस्सी वर्ष पुरानी कौनेक ब्रैण्डी, रेज़िडेण्ट की पत्नी के लिए हरी क्रीम डी० मिंथ, पौलिटिकल एजेण्ट के लिए विशेष रूप से बनायी गयी कॉकटेल, बर्फ के ऊँचे अम्बार में खनकती बियर बड़े कायदे से निकाली जातीं। कभी भी सस्ती ही-ही ठी-ठी या उल-जलूल बातों को सुनने का अवसर नहीं आता। हम सब बहुत छोटे थे। डॉ० कुरेशी, सर गिरजाशंकर बाजपेयी, सर सुल्तान अहमद अभी पिताजी के विशेष मित्रों में थे। एक बार प्रख्यात पहलवान राममूर्ति भी हमारे अतिथि होकर तीन दिन रहे और उनका नाश्ता देखकर, हम बच्चें स्तम्भ रह गए थे। एक लोहे की मोटी जंजीर को, जिससे हमारी हथिनी-सी हिसार की भैंस को बाँधा जात था, उन्होंने अपनी दौ ही अंगुलियों में मसलकर, लोहे का गोल बना दिया था। मेरा भाई राजा कहता था कि वे नीम के पेड़ जड़ से उखाड़कर दतौन किया करते हैं। मैंने उसकी बात पर बड़े भोलेपन से विश्वास कर लिया और एक बार उनसे दतौन क्रिया-प्रदर्शन का अनुरोध किया तो वे ठठाकर हँस पड़े : ‘तुम्हारा भाई बहुत बड़ा गप्पी बनेगा उन्होंने कहा था। सचमुच उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। अब तक वह एक सफल पत्रकार बन चुका है।
इसी बीच हमारी सुनहली सल्तनत हमसे सहसा छीन ली गयी। दादाजी के बार-बार आग्रह करने पर हमें अल्मोड़ा भेज दिया गया। अल्मोड़ा पहुँचने के कुछ ही दिन बाद ईद पड़ी थी। पहाड़ की ईद पर एक छोटा मोटा मेला भी लगता था, हम देखने गये, तो कलेजा उमड़ आया। कहा रामपुर की ईंद, कहाँ पहाड़ की ! सुबह उठते ही रामपुर के ओर-छोर रंगीन हो उठते थे। नागलदोले की घर्र-घर्र, बीन, गुब्बारों की चीं-चीं, साथ ही हिन्दू होने पर भी हम भाई-बहन नये जोंड़ों के दिलपसन्द और गुलबदन की रेशमी फुलझड़ियाँ छोड़ते, मेला देखने के चल पड़ते।
बड़ी मस्जिद के पास दूधिया मीनारें, एक साथ सिजदे में उठती, झुकती पीठें, मस्जिद के बाहर नये चमकते जूतों की एक लम्बी कतार, हम मन्त्रमुग्ध होकर देखते-देखते नवाज खत्म होने पर पिताजी के स्टेनो अहब साहब हमें मेला दिखाने ले चलते, मुख्य आकर्षण रहता साढ़े पांच आने की दुकान में, जहाँ दुरबीन से ले रेशमी रूमाल, गुड़ियों के कटोरदान से लेकर सुरमेदानी-सब कुछ साढे पाँच आने में मिलता था। पहले-पहले हम दोनों भाई-बहन-अपना प्रिवी पर्स अलग रखते, पर फिर जब दोनों की आर्थिक हालत बहुत दुविधा में नहीं रहती, तो मूलधन मिला दिया जाता। दिन डूबे मेले से लौटते तो अगली ईद का इन्तजार रहता, पर अल्मोड़े की फीकी ईंद ने हमें उदास कर दिया। उधर हमारे सनातनी पितामह ने अपने अनुशासन की पकड़ और कड़ी कर दी थी। हमारी शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर दिया गया था। सुबह उठते ही संस्कृत के पण्डित गंगादत्त जी आ जाते। नित्य उन्हें अमरकोश के पाँच श्लोक कण्ठस्थ कर सुनाने होते। फिर तीनों भाई-बहनों को लाइन में खड़ा कर त्रिफला से आँखें धुलवाई जातीं। चालीस वर्ष के अनुसाशन की लगाम में गृह के अनेक सदस्यों को कसते-कसते, लोहनीजी दक्ष हो गये थे। जरा भी चींचपड़ की तो हाथ-पैर बँधकर लकड़ी की कोठरी में डाल देते और हफ्ता-भर मूली, लौकी, कद्दू-जैसी अरसिया सब्जियाँ खिला-खिलाकर नाक में दम कर देते।
सुबह उनके साथ घूमने जाना अनिवार्य था। सद्यःस्नाता कुमाऊँ की अनुपम वनस्थली का वह रूप आज भी मेरी कलम की स्याही जुटाता रहता है। लम्बे चीड़, देवदार और अयार के वृक्षों से लटकते ओस की बूँदों के मोती-जड़े लटकन टप-टप बिखर कर हमें भिगों देते। और लौटते तो गिरजे की घण्टियाँ बज रही होतीं। पता नहीं क्यों गिरजे की घण्टियों की जो मिठास, अल्मोड़ा के गिरजे में है, वह मुझे अन्य कहीं नहीं लगता है अल्मोड़ा का सरल, स्निग्ध सौन्दर्य, घण्टें की मिठास में घुल-मिल गया है। कभी तिब्बती चरवाहे, अपनी भेड़ों के झुण्ड को ‘हे हो’ कर हाँकते पूरी सड़क घेर लेते और उनके भालू-से कद्दावर ‘अप्सु’ जात के कुत्तें अपनी लाल आँखों से हमें घूरते-सूँघते चले जाते। वही सड़क पर एक बार हम दोनों बहनों ने, दो सुन्दर तिब्बती लड़कियों से बहनापा भी जोड़ा था। रोम, जिसकी दसों अंगुलियों में याकूत और फिरोजा की अँगूठियाँ थीं, जो हँसने पर दोनों आँखें मूंद लेती थीं, और पुट्टी जो अपनी उदास बटन-सी आँखों को दमकती होंठों-ही-होठों में ‘ओ मनी पद्म हूँ’ जाप करती रहती थी। लोहनीजी के घर पहुँचने पर हमें गोमूत्र से पवित्र करके खूब लताड़ा था। ‘जाने किन म्लेच्छ, अघोरी लम्याणियों से दोस्ती पाल आयी है, खबरदार जो उन्हें घर बुलाया। ऐसी छोकरियाँ जादू-टोना जानती है।’ पर उनके आदेश को हमने हँसी में उड़ा दिया था और पिछवाड़े के द्वार से कई बार रोमा, पुट्टी को अपने कमरे में बुला लिया था। बाद में तराई में, रामा को पागल कुत्तें ने काट लिया और वह सुना भौंकती-भौंकती मर गयी। पुट्टी को हमने फिर कभी नहीं देखा, क्या पता अब भी तिब्बती के किसी रहस्यमय मठ में ओठों-ही-ओठों में बुदबुदाती जा रही होगीः ‘ओ मनी पद्म हुं।
‘चुप छोकरी’, वे धमक लगाकर फिर झूमने लगते।
‘असल में बूढ़ज्यू को शिव की स्तुति आती नहीं’, मेरा भाई कहता और हम दोनों भाव-विभोर लोहनीजी के साथ बड़ी देर तक आरती गाते रहते। मांणावदर रहने के पश्चात् रामपुर में पिताजी की नियुक्ति हुई गृहमन्त्री के पद पर। मेरे पितामह, काशी विश्वविद्यालय में धर्म-प्रचारक के पद पर थे। वे कुमाऊँ के पहले ग्रेजुएट थे, साथ ही संस्कृति के धुरन्दर विद्धान् और और दबंग वकील। उन्हें पिताजी की इस ऊँची नौकरी के प्रसन्नता नहीं हुई। मालवीयजी की इच्छा नहीं थी कि पिताजी रामपुर जायें, वे मेरे पितामह के अन्तरंग मित्र थे और उनसे सलाह लेकर मेरे पितामह ने पिताजी को राजकोट ही रहने दिया; पर तब तक हम सब रामपुर आ चुके थे।
हम भाई-बहनों की साहबी शिक्षा भी पितामाह के आदर्शों के विपरीत हो रही थी। बड़े-भाई के लिए नैनिताल में एक बँगला ले दिया था, वहीं एक अंग्रेज गवर्नेस मिस स्मिथ से पढ़ने नित्य उनके बँगले में जाना पड़ता था। मि० स्मिथ विलायत से पहली बार भारत आये थे, इसी से पति-पत्नि को हिन्दी एकदम ही नहीं आती थी। कभी-कभी वे दोनों नये शब्द का हिन्दी उल्था लिखने ही में पूरा समय बिता देते। सुबह 6 बजे, मुझे घुड़सवारी सिखाने आते बूढे़ सिकन्दर मियाँ उनके राख के रंग के लहकदार साफे की लम्बी चोटी उनकी चौड़ी पीठ पर भरतनाट्यम की नर्तकी के पंख-सी बड़ी अन्दाज से फैली रहती। उनकी मेंहदी से रँगी दाढ़ी और मूछों के संगम पर, पान के छींटे फुलकारी-सी किये रहते।
‘इन्शाअल्ला, बिट्टो, तुम अब घुड़सवारी में किसुनभैया को भी पछाड़ सकती हो’, वे कहते और मैं गर्व से फूल उठती। किसुनभैया के पिता श्री बृजचन्द्र शर्मा मेरे पिता जी अभिन्न मित्र थे और वहीं रेवेन्यू मिनिस्टर थे। एक दिन कुआँ फाँदने की हर्डल में मैंने सचमुच ही ‘किसुन भैया’ को हरा दिया, तो सिकन्दर मियाँ ने मेरा माथा चूम लिया। तब मैं सचमुच ही उनके बाजी मार ले गयी थी, पर जिन्दगी की दौड़ में घोड़ा भगाते अब मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं। कुछ वर्ष पूर्व पेंकिग में एक उच्च पदस्थ फौजी अफसर थे। अपने फौज़ी बिल्लों के बीच अब तो शायद कई सोने के तमगे लटका चुके होंगे, पर भाग्य की विडम्बना देखिए कि वर्षों पहले उन्हें घुड़सवारी में पछाड़ने पर आज तक मैं एक तमगा भी नहीं जुटा पायी।
हमारे बँगले का नाम था : ‘मुस्तफा लॉज। बँगला क्या, अच्छा-खासा इमामबाड़ा था। लाल ईंटों की बनी वह भव्य कोठी वर्षों से होम साहब की कोठी राही थी। उनके सामने बहुत बड़ा मखमली लॉन था। मेहराबदार ड्योढ़ी में चार-चार सन्तरी, ऊँची संगीनें उठाये दिन-रात सख्त पहरा देते थे। उन दिनों हिन्दू होम साहब की सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध रहता था। बाग में रंगीन क्यारियों में नीले, ऊदे फूलों को घेरे मेंहदी में ऊँची बाड़ को, सरूपा माली दिन-रात तर किये रहता। भींगी मेंहदी की मीठी खुशबू-इश्कपेंचा की बेल पर चढती, पूरे छज्जे पर फैल जाती है; जहाँ तख्त लगाकर मशीन घरघराता मूलचन्द्र दर्जी हमारे लिए चक्की के पाट-सी पायंचो की सलवारें और रामपुर के खास चुन्नट पड़े ढीले कुर्तें सिलता, जिनकी बाँहों में हीना और खस की चुटकियाँ भरने, काने चमन मियाँ अपनी एक आँख के ज्योतिपुंज का जुगनू चमकते सहस्त्र चुन्नटें डालते। आज भी आँखें बन्द करके उस बिसरी सुगन्ध की स्मृति के नथुनों भींचकर सूंघने की चेष्टा करती हूँ, पर कुछ भी हाथ नहीं लगता।
हमारे दीवानखाने में चारों ओर किताबों का अम्बार चुना रहता, घर का पत्येक व्यक्ति पढ़ने के पीछे दीवाना था, यहाँ तक कि बूढ़ें लोहनीजी भी बिना पढ़े नींद नहीं आती थी। हमारी माँ की गुजराती पुस्तकों का भण्डार नित्य नवीन रहता। मुंशी, मेघाणी उनके प्रिय लेखक थे। एक बार छिपाकर ‘सरस्वतीचन्द्र’ पढ़ने पर माँ का जो करारा चाँटा पड़ा था। वह भी नहीं भूलता।
अतिथियों का मेला नित्य लगा ही रहता। पिताजी अपने आतिथ्य और ऊँची पसन्द के ‘सेलर’ के लिए प्रसिद्ध थे। अस्सी वर्ष पुरानी कौनेक ब्रैण्डी, रेज़िडेण्ट की पत्नी के लिए हरी क्रीम डी० मिंथ, पौलिटिकल एजेण्ट के लिए विशेष रूप से बनायी गयी कॉकटेल, बर्फ के ऊँचे अम्बार में खनकती बियर बड़े कायदे से निकाली जातीं। कभी भी सस्ती ही-ही ठी-ठी या उल-जलूल बातों को सुनने का अवसर नहीं आता। हम सब बहुत छोटे थे। डॉ० कुरेशी, सर गिरजाशंकर बाजपेयी, सर सुल्तान अहमद अभी पिताजी के विशेष मित्रों में थे। एक बार प्रख्यात पहलवान राममूर्ति भी हमारे अतिथि होकर तीन दिन रहे और उनका नाश्ता देखकर, हम बच्चें स्तम्भ रह गए थे। एक लोहे की मोटी जंजीर को, जिससे हमारी हथिनी-सी हिसार की भैंस को बाँधा जात था, उन्होंने अपनी दौ ही अंगुलियों में मसलकर, लोहे का गोल बना दिया था। मेरा भाई राजा कहता था कि वे नीम के पेड़ जड़ से उखाड़कर दतौन किया करते हैं। मैंने उसकी बात पर बड़े भोलेपन से विश्वास कर लिया और एक बार उनसे दतौन क्रिया-प्रदर्शन का अनुरोध किया तो वे ठठाकर हँस पड़े : ‘तुम्हारा भाई बहुत बड़ा गप्पी बनेगा उन्होंने कहा था। सचमुच उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। अब तक वह एक सफल पत्रकार बन चुका है।
इसी बीच हमारी सुनहली सल्तनत हमसे सहसा छीन ली गयी। दादाजी के बार-बार आग्रह करने पर हमें अल्मोड़ा भेज दिया गया। अल्मोड़ा पहुँचने के कुछ ही दिन बाद ईद पड़ी थी। पहाड़ की ईद पर एक छोटा मोटा मेला भी लगता था, हम देखने गये, तो कलेजा उमड़ आया। कहा रामपुर की ईंद, कहाँ पहाड़ की ! सुबह उठते ही रामपुर के ओर-छोर रंगीन हो उठते थे। नागलदोले की घर्र-घर्र, बीन, गुब्बारों की चीं-चीं, साथ ही हिन्दू होने पर भी हम भाई-बहन नये जोंड़ों के दिलपसन्द और गुलबदन की रेशमी फुलझड़ियाँ छोड़ते, मेला देखने के चल पड़ते।
बड़ी मस्जिद के पास दूधिया मीनारें, एक साथ सिजदे में उठती, झुकती पीठें, मस्जिद के बाहर नये चमकते जूतों की एक लम्बी कतार, हम मन्त्रमुग्ध होकर देखते-देखते नवाज खत्म होने पर पिताजी के स्टेनो अहब साहब हमें मेला दिखाने ले चलते, मुख्य आकर्षण रहता साढ़े पांच आने की दुकान में, जहाँ दुरबीन से ले रेशमी रूमाल, गुड़ियों के कटोरदान से लेकर सुरमेदानी-सब कुछ साढे पाँच आने में मिलता था। पहले-पहले हम दोनों भाई-बहन-अपना प्रिवी पर्स अलग रखते, पर फिर जब दोनों की आर्थिक हालत बहुत दुविधा में नहीं रहती, तो मूलधन मिला दिया जाता। दिन डूबे मेले से लौटते तो अगली ईद का इन्तजार रहता, पर अल्मोड़े की फीकी ईंद ने हमें उदास कर दिया। उधर हमारे सनातनी पितामह ने अपने अनुशासन की पकड़ और कड़ी कर दी थी। हमारी शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर दिया गया था। सुबह उठते ही संस्कृत के पण्डित गंगादत्त जी आ जाते। नित्य उन्हें अमरकोश के पाँच श्लोक कण्ठस्थ कर सुनाने होते। फिर तीनों भाई-बहनों को लाइन में खड़ा कर त्रिफला से आँखें धुलवाई जातीं। चालीस वर्ष के अनुसाशन की लगाम में गृह के अनेक सदस्यों को कसते-कसते, लोहनीजी दक्ष हो गये थे। जरा भी चींचपड़ की तो हाथ-पैर बँधकर लकड़ी की कोठरी में डाल देते और हफ्ता-भर मूली, लौकी, कद्दू-जैसी अरसिया सब्जियाँ खिला-खिलाकर नाक में दम कर देते।
सुबह उनके साथ घूमने जाना अनिवार्य था। सद्यःस्नाता कुमाऊँ की अनुपम वनस्थली का वह रूप आज भी मेरी कलम की स्याही जुटाता रहता है। लम्बे चीड़, देवदार और अयार के वृक्षों से लटकते ओस की बूँदों के मोती-जड़े लटकन टप-टप बिखर कर हमें भिगों देते। और लौटते तो गिरजे की घण्टियाँ बज रही होतीं। पता नहीं क्यों गिरजे की घण्टियों की जो मिठास, अल्मोड़ा के गिरजे में है, वह मुझे अन्य कहीं नहीं लगता है अल्मोड़ा का सरल, स्निग्ध सौन्दर्य, घण्टें की मिठास में घुल-मिल गया है। कभी तिब्बती चरवाहे, अपनी भेड़ों के झुण्ड को ‘हे हो’ कर हाँकते पूरी सड़क घेर लेते और उनके भालू-से कद्दावर ‘अप्सु’ जात के कुत्तें अपनी लाल आँखों से हमें घूरते-सूँघते चले जाते। वही सड़क पर एक बार हम दोनों बहनों ने, दो सुन्दर तिब्बती लड़कियों से बहनापा भी जोड़ा था। रोम, जिसकी दसों अंगुलियों में याकूत और फिरोजा की अँगूठियाँ थीं, जो हँसने पर दोनों आँखें मूंद लेती थीं, और पुट्टी जो अपनी उदास बटन-सी आँखों को दमकती होंठों-ही-होठों में ‘ओ मनी पद्म हूँ’ जाप करती रहती थी। लोहनीजी के घर पहुँचने पर हमें गोमूत्र से पवित्र करके खूब लताड़ा था। ‘जाने किन म्लेच्छ, अघोरी लम्याणियों से दोस्ती पाल आयी है, खबरदार जो उन्हें घर बुलाया। ऐसी छोकरियाँ जादू-टोना जानती है।’ पर उनके आदेश को हमने हँसी में उड़ा दिया था और पिछवाड़े के द्वार से कई बार रोमा, पुट्टी को अपने कमरे में बुला लिया था। बाद में तराई में, रामा को पागल कुत्तें ने काट लिया और वह सुना भौंकती-भौंकती मर गयी। पुट्टी को हमने फिर कभी नहीं देखा, क्या पता अब भी तिब्बती के किसी रहस्यमय मठ में ओठों-ही-ओठों में बुदबुदाती जा रही होगीः ‘ओ मनी पद्म हुं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book











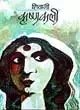
_s.webp)