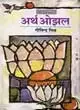|
सांस्कृतिक >> कोहरे में कैद रंग कोहरे में कैद रंगगोविन्द मिश्र
|
777 पाठक हैं |
||||||
समकालीन साहित्य में अपनी अलग पहचान बनानेवाले विख्यात कथाकार गोविन्दमिश्र का नवीन उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘कोहरे में कैद रंग’ - जीवन के विविध रंग ? रंग ही रंग हर व्यक्ति का अपना अलग रंग... जिसे लिये हुए वह संसार में आता है। अक्सर वह रंग दिखता नहीं, क्योंकि वह असमय ही कोहरे से घिर जाता है। कुछ होते हैं जो उस रंग को अपने जीवन-शैली में गुम्फित कर लेते हैं। काश उन ? रंगों पर कोहरे की चादर न होती तो जाने कैसा हुआ होता वह रंग ! तरह-तरह के रंगों से सजी जीवन की चादर हमारे सामने फैलाता है यह उपन्यास। विषम परिस्थितियों में भी गरिमा से जीते लोग, अपना-अपना जीवन-धर्म निबाहते हुए, और इस तरह अपनी तथा आज के पाठक की जीवन के प्रति आस्था को और दृढ़ करते हुए...
अपने पूर्व उपन्यास ‘फूल.... इमारतें और बन्दर’ में जहाँ गोविन्द मिश्र की दृष्टि समय विशेष के यथार्थ पर अधिक थी, ‘कोहरे में कैद रंग’ तक आकर वह यथार्थ-आदर्श, बाह्य-आन्तरिक जैसे कितने ही द्वन्द्वों से बचती हुई एक संतुलित जीवन-बोध देती है। जीवन, सिर्फ जीवन-जिसका रंग पानी जैसा है, काल-सीमाओं से पार एक-सा बहता हुआ... करीब-करीब।
अपने पूर्व उपन्यास ‘फूल.... इमारतें और बन्दर’ में जहाँ गोविन्द मिश्र की दृष्टि समय विशेष के यथार्थ पर अधिक थी, ‘कोहरे में कैद रंग’ तक आकर वह यथार्थ-आदर्श, बाह्य-आन्तरिक जैसे कितने ही द्वन्द्वों से बचती हुई एक संतुलित जीवन-बोध देती है। जीवन, सिर्फ जीवन-जिसका रंग पानी जैसा है, काल-सीमाओं से पार एक-सा बहता हुआ... करीब-करीब।
कोहरे में कैद रंग
अमरकण्टक-मध्यप्रदेश में एक छोटी-सी नगरी, भारत में अपनी तरह की अनूठी-जहाँ से दो बड़ी नदियाँ निकलती हैं- सोन और नर्मदा, निकलकर दो विपरीत दिशाओं में बहती हुई। सोन नद, नर्मदा नदी-प्रेमी और प्रेमिका, पर नियति कि दोनों विपरीत दिशाओं में चले फिर कभी न मिलने के लिए। छोटा-सा संयोग, फिर वियोग ही वियोग। हाय जीवन।
नर्मदा एक छोटे से कुण्ड में प्रकट होती है। नीचे गिरते ही उसकी क्षीण धारा को एक धर्मकुण्ड में कैद कर लिया गया है जिसमें लोग पुण्य कमाने के नाम पर नहाते और गन्दगी मचाते हैं। जलाशय का पानी एक सड़क के नीचे से उतरकर एक तरफ निकलता है तो वे उसके इर्द-गिर्द शौच को बैठ जाते हैं, जैसे जहाँ नदी दिखाई दी कि गन्दा करने के लिए झपट पड़े हमारे भक्त, तीर्थयात्री, नगरवासी, भारतवासी। बेचारी नदी नाली की तरह किसी तरह आगे चली तो नगरियों ने उसे फौरन एक छोटे बाँध में बाँध तालाब बना लिया-मुँह धोने, खँखारने कपड़े धोने और नौका विहार कराकर पैसा कमाने के लिए। नर्मदा अपने को किसी तरह छुड़ा कीचड़वाली नाली की शक्ल में आगे खचुरती, अपने जल को कीचड़ के ऊपर धीरे-धीरे बहाती आगे बढ़ती है। फिर प्रवाह तेज होने लगता है, जैसे जान बचाकर आदमी की बस्ती से दूर भाग जाना चाहती हो। बस्ती के बाहर पहुँचते ही वह कपिलधारा बनकर खूब नीचे, खाई में पत्थरों के ऊपर गिरती है...अपने को तोड़ते हुए, गन्दगी को निकालते, स्वयं को निथारते हुए। यहाँ से दोनों तरफ पहाड़ की सुरक्षा है-आगे, काफी दूर तक। अब जहाँ तक हो सकेगा वह आदमी की बस्ती से दूर-दूर चलना चाहेगी, ताकि खुद को शुद्ध रख सके, उसे अपने से ही दुर्गन्ध न आने लगे, लेकिन यह शातिर चीज आदमी, जहाँ नर्मदा होगी, वहाँ पहुँच जाएगा, घर बैठा लेगा, बस्ती जमा लेगा, गन्दगी फैलाएगा...कहेगा कि उसके धर्मतीर्थ हैं, जबकि देखो तो धर्म तुममें कहाँ, नर्मदा में है। नर्मदा से तुम्हें अपने में उतारना है। पर तुम तो उसी को नष्ट करने पर तुले हुए हो। नर्मदा और भारतीय नारी में कितनी समानता है।
नर्मदा ने शुरूआत में ही एक सीख ले ली, कपिलधारा बनते ही-जब-जब तुममें गन्दगी इकट्ठा हो जाए, पहाड़-पत्थरों पर खुद को दे मारो, स्वयं को पछीटते चलो, रेशा-रेशा, कण-कण। इसी तरह तुम खुद को साफ रख सकते हो। नर्मदा की यात्रा कैद से निकलकर बहने, प्रपात बनकर गिरने, फिर बहने की है। जहाँ कूड़ा-कचरा, दिखावा-पाखण्ड, नोचना-खसोटना हुआ वहाँ उथली होकर ऊपर-ऊपर से निकल जाओ, जहाँ स्वच्छता प्रेम पाओ वहाँ रम जाओ, गहरी हो जाओ, धीरे-धीरे बहो...।
सोन नद चतुर है, कुण्ड से निकलते ही भागने लगता है, ढलानों में इधर से, उधर से..इतनी पतली धारा में कि दिखाई भी न दे..और मुश्किल से सौ गज आगे जाकर नीचे कूद जाता है, कूदकर तिरोहित हो जाता है, फिर आसानी से पकड़ में नहीं आता। पुरुष है !
मुझे नर्मदा की कहानी सृजन की कहानी भी लगती है-लिखना माने अपने को बचाये रखने, शुद्ध करने के क्रम में निरन्तर स्वयं को तोड़ते चलना, तरह-तरह से बहना। रचनाओं-प्रपातों में गिरने से प्राणवायु निर्मित होती है, जो स्वयं को तो जीवित रखती ही है, वातावरण में भी बिखरती है। मनुष्य जाति, समाज की गन्दगी न भी धुल पाये तो कुछ के अन्तर्मन तो निर्मल हुए, आसपास का वातावरण तो शुद्ध हुआ। जरूरत हुई तो नर्मदा विध्वंसकारी रूप भी धारण करती है।
जो सृजन का सच है वही क्या जीवन का सच भी नहीं ? धरती पर हमारे आते ही समाज की गन्दगी, उसकी जंग लगी संस्थाएँ, रूढ़ियाँ जड़ विचार हमें अपने आगोश में लेने को दौड़ते हैं, हमें नष्ट कर देने को आतुर। भयभीत हम भागते हैं खुद को बचाने के लिए। बच सके यही क्या कम है ! खुद को, अपने आसपास के लोगों को जीने में आस्था दे सके तो यह उसका कितना अच्छा प्रतिदान हुआ, जिसे कुछ लोग अपने जीवन की तमाम विषम परिस्थितियों के बीच, अपने जीवन संघर्ष के साथ-साथ हमारे लिए कर गये-अनायास। वे जो हमारे सामने जीवित थे, उनके प्रति हम अपने अनुग्रह को ठीक से प्रकट भी नहीं कर सके थे। हम वह नहीं कर पाये तो यह तो कर सकते हैं कि उन लोगों की स्मृति को अपने जीवन में लौटा-लौटा कर लाएँ, उनकी सुगन्ध को बाहर बिखेंरे।
मुझमें कितना मेरा अपना है ? जो है वह भी मेरा कहाँ ! कहीं से आया होगा, जिसे मैंने तराश कर वह बनाया, जिसे आज अपना कहता हूँ। इस पोटली को कलेजे से लगाये चल रहा हूँ। चल रहा हूँ या कि भाग रहा हूँ ? तेजी से बीत तो रहा ही हूँ। मेरी यात्रा समाप्ति की ओर है, लेकिन नर्मदा समाप्त नहीं होती, सागर में समा जाती है। और उसका चलना, बहना भी अनवरत है-जाती हुई जलधारा के पीछे आती असंख्य जलधाराएँ, एक-पर-एक। क्या ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है या कि मेरा चलना-बहना मेरे जीवन के साथ ही समाप्त हो जाएगा ? वह अनवरत हो सकता है अगर उसमें उनका बहना समाहित हो जाए जो मेरे आगे गये, जो मेरे पीछे बहेंगे..अनवरत बहती मानव जलधारा !
मनुष्य को यह सिफत मिली है कि जो पीछे छूट गया वह उसे देख सकता है..काफी कुछ। बीत हुए का सत्त्व निकाल सकता है। अपने चलने-बहने को कोई उसी वक्त देखता चल सकता है क्या ? शायद हाँ, कोशिश करके...थोड़ा-बहुत। जो वह जी रहा है उसके परे कितना कुछ है वह भी दिख सकता है-विलक्षण क्षणों में। अपनी और अपनों की जीवन कहानियाँ कह, उनके तनावों-द्वन्द्वों का खुलासा कर वह असंख्य जलधाराओं की सृष्टि कर सकता है जिनके आलोक में आने वाले लोग भी अपना बहना देख सकें।
नीम की डगाल से लटका मूँज की डोरियों का बना एक छींका, जिस पर रखी थी रसखीर, लाल रंग मिट्टी की चपिया में, ढकना भी मिट्टी का। शाम पिता ने अपने आठ साल के लड़के के लिए गन्ने का रस मँगाया था और कण्डों के ऊपर रोटी-दाल के बाद मिट्टी की इस चपिया में खुद खीर पकायी थी। रात के खाने के बाद जो बची उसे उन्होंने छींके पर टाँग दिया था, बिल्ली से बचे और रात भर चाँदनी की ठण्डक चपिया में पहमती भी रहे।
गोल-गोल बड़े चबूतरे पर नीम का वह पेड़ खासा बड़ा और छायादार था। दिन में वहाँ उस गाँव की एकमात्र प्राथमिक पाठशाला लगती जिसमें पिता अकेले शिक्षक थे। रात को उसी चबूतरे पर दो खटियाँ बिछी थी। चाँदनी की छोटी-बड़ी बुन्दकियाँ चबूतरे पर फैली थीं। ऊपर नीम की पत्तियाँ हल्के-हल्के डोलतीं, पत्तियों के पार तारे टिमटिमाते थे। तारों में मैं सप्तर्षि खोजता रहा। दिखाई दिये तो मैंने गिने-पूरे सात। फिर नजर डगाल से लटके छींके पर अटक गयी-रसखीर..आसमान और जमीन के बीच। मेरा ध्यान उसी में था, विश्वास भी था कि कल मिलेगी। यह समझ नहीं थी कि खीर तो कल खत्म भी हो जाएगी, पेड़ के ऊपर तारे..वे कभी न मिलेंगे, पर बराबर रहेंगे।
थोड़ी दूर पर पिता की चारपाई थी। बीच में पानी का एक घैला और एक लुटिया। नीम का यह पेड़ ही पिता का घर था। जाड़े-बरसात में वे स्कूल की जो एकमात्र कोठरिया थी, वहाँ चले जाते। कोठरिया में एक किनारे एक टूटी-सी लकड़ी की सन्दूकची में रखी उनकी पूरी गृहस्थी-दो धोती, एक लाल गमछा, दो कुर्ते, आटा-दाल की कुछ मोटी-मोटी कन्सरियाँ, कुछ डिब्बे। सन्दूकची के ऊपर रखा रहता एक छोटा-सा पीतल का सिंहासन, जिसके ऊपर चाँदी का एक छोटा छत्र था। सिंहासन में दो छोटे-छोटे शालिग्राम के बीच एक छोटे से बालमुकुन्द जिनके नाक-नक्श मुश्किल से दिखाई देते थे।
चबूतरे के नीचे गाँव की बड़ी गली थी जो बाहर से गाँव में आती थी और गाँव के बाहर निकलती थी। नींद आने तक वहाँ से जब-तब उठती चमरौधों की चर्म-मर्र सुनाई देती रही।
अगली सुबह कण्डों पर ही पिता ने खाना बना दिया-मूँग की दाल, रोटी और कण्डों की बुझती आग में भुने हुए आलू जिन्हें छिलके समेत मीस, नमक-मिर्च-प्याज मिला भरता बना लिया गया। सबसे बाद में रसखीर जो चाँदनी पीकर अमृत हो गयी थी।
पिता मुझसे मतलब की ही बात बोलते थे। मैं अब सोच सकता हूँ कि अपने बारे में वे जानते थे कि उनकी जुबान कर्कश थी, कड़वे बोल मुझ तक नहीं पहुँचाना चाहते थे, खासतौर से तब, जब वे मुझे कस्बे से अपने गाँव एक दिन के लिए लाये थे-इसको लेकर वे सजग थे। वे गाँव में पढ़ाते थे, माँ कस्बे में। मैं कस्बे के स्कूल में पढ़ता था। पिता इतवार के इतवार कस्बे आते थे, कभी-कभी नहीं भी आते थे।
दस बजे से पाठशाला लग गयी। लड़के (लड़कियाँ नहीं थीं) मैली-कुचैली पोशाक में, कोई-कोई कमीज से नाक पोंछते, सब पाटी बोरका के साथ चबूतरे पर फैल गये। रात चबूतरे पर चाँदनी की नीरवता और शीतलता थी, अब जैसे सुबह के पक्षियों का कलरव और गर्मी। पिता ने मेरे लिए दो-चार लड़कों को पहाड़े लिखवाने और जाँचने का काम सौंप मुझे थोड़ी देर का छोटा-मोटा मास्टर बना दिया। दोपहर के थोड़ा बाद छुट्टी कर दी गयी और पिता मुझे कस्बे वापस भेजने चल दिये। चलने से पहले उन्होंने फिर खाने को दिया-सवेरे की बची रोटियाँ, भुने आलुओं का भर्ता। उनका सिद्धांत था-कहीं जाने के पहले पेट जरूर भर लो, वर्ना चलोगे कैसे और पता नहीं खाना कब और कहां मिले। खाने के बाद हमने भरपेट पानी पिया और निकल पड़े।
बैलगाड़ी वाले रास्ते के किनारे-किनारे पिता चले जा रहे थे। मैं उनसे हमेशा पीछे रह जाता, फिर उनकी बराबरी पर आ जाने के लिए दौड़ता। पीछे से दिखाई देती थीं धोती के नीचे खुलती उनकी टाँगें-दुबली पर सुडौल बराबर चलती टाँगें..जो न तेज होती थीं, न पिछड़ती थीं, चलती चली जाती थीं, चलती चली जाती थीं। रास्ते में एक कुएँ पर रुककर उन्होंने झोले से लोटा-डोर निकाली। कुएँ से लोटे में पानी निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने एक हाथ की चुल्लू बनायी, एक हाथ से लोटे का पानी उसमें डालता गया, पीता गया। मीठा पानी ठण्डा पृथ्वी के गर्भ से खास मेरे लिए निकला पानी। साफ, ऊर्जा भर देने वाला सिर्फ उतना जितनी मुझे जरूरत थी।
पिता आधे रास्ते तक पहुँचा गये। उसके आगे का रास्ता मुझे ठीक से समझा दिया-‘बैलगाड़ी के इसी रास्ते को पकड़े रहना, जब एक बड़ा बगरद का पेड़ मिले तो बायें मुड़ जाना। एक मोटी पगडण्डी होगी वह, जो सीधे पहाड़ी की जड़ तक ले जाएगी। फिर पहाड़ी की सीढ़ियाँ पकड़ लेना, सीढ़ियाँ पहले ऊपर चढ़ेंगी हरी तलैया तक, फिर उतरेंगी। उतरते ही अपनी बस्ती आ जाएगी।’ उसके बाद मैं आगे की तरफ चला वे वापस उस गाँव की ओर लौट पड़े जहाँ से हम चले थे।
मैं पीछे मुड़-मुड़कर पिता को गाँव लौटते देखता रहा। धोती के नीचे झलकती उनकी टाँगों को भी। उन्होंने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, या शायद देखा हो जब मैंने न देखा हो।
पहाड़ की जड़ तक मैं तेज चला, पहाड़ की सीढ़ियों पर हाँफते हुए। सीढ़ियों की चढ़ाई जहाँ खत्म हुई वहाँ हरी तलैया मिली। पानी के ऊपर उतराती हरी काई, नीचे पानी भी हरा। तलैया पर चारों तरफ से घिरी पहाड़ियों की हरियाली का अक्स पड़ता था, शायद इसलिए पानी हरा दिखता था। मैं तलैया की पट्टी पर थोड़ी देर सुस्ताने बैठा। सामने सीढ़ियों पर कपड़े फींचती एक औरत, काई हटाकर डुबकी मारता एक बूढ़ा आदमी, ऊपर वाली सीढ़ी से कूदते, तैरकर घाट तक वापस आते दो-तीन मेरी उम्र के बच्चे। इस तरफ के घाट पर आठ-दस आदमी डुबकी लगाकर एक-एक कर बाहर निकल रहे थे, निकलकर भीगे कपड़े पहनते हुए।
वहाँ से रास्ता थोड़ी दूर तक बड़े पत्थरों पर से चला, फिर छोटे सपाट पत्थरों पर से नीचे लुढ़कने लगा। चलने वाला मैं अकेला। तभी सामने से कुछ, लोग मेरी तरफ आते दिखे। ‘राम नाम सत्य है’ की मिली-जुली मद्धिम आवाज-जितनी एकरस, उतनी ही डरावनी। चार-छः लोग एक अरथी को उठाए थे। नीचे उठंग धोती, ऊपर नंगा बदन, सिर या कन्धों पर लाल गमछा। मैं डरकर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। दस-पन्द्रह लोगों की वह छोटी-सी टुकड़ी ‘राम नाम सत्य’ करती ज्यों-ज्यों मेरे पास आती जा रही थी, मेरी धुकधुकी बढ़ती जाती थी। जब वह मेरे बगल से गुजरी तो मेरे चारों तरफ डर का घटाटोप-ऊपर सूना आसमान, नीचे उतरती शाम की छाया, चारों तरफ पहाड़, बीच के रास्ते में बड़े-बड़े पत्थर, जिन पर से गुजरती वह शवयात्रा और एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा मैं।
कहां जा रहे थे ये लोग, किसको ऊपर बांधे ? उन सबके चेहरे, स्वर चाल सब एक तरह के और संजीदा क्यों थे। मैं सोच रहा था।
लोग मरते हैं यह तो मैं जानता था लेकिन यह नहीं जानता था कि क्यों मरते हैं। लोगों की टोली निकल गयी। मैं सपाट पत्थरोंवाले रास्ते पर आ गया तो सामने से एक वृद्धावस्था को छूता आदमी, उघारे बदन, रोता-बिलखता दौड़ता चला आ रहा था। उसके आँसू और आवाज दोनों सूख गये थे। चेहरे पर ऐसी वेदना, ऐसी असहायता-जैसे उसका सबकुछ लुट गया हो। आधा पागल, बदहवास वह अरथी के पीछे दौड़ा चला जा रहा था जैसे भैंस दौड़ती है, जब उसके छोटे मरे बच्चे को उठाकर ले जाते हैं।
वह पहली शवयात्रा थी जो मैंने देखी, अकेले। इसके पहले घर के बाहर से गुजरती कई शवयात्राओं की झलक दिखी थी, माँ दौड़कर किवाड़ बन्द कर लेती थीं। पिता ने मुझे उस रास्ते से भेजा जहाँ पास में श्मशान था, हरी तलैया थी जहाँ शवयात्रा से लौटकर लोग नहाते थे।
कुछ फर्क पड़ता क्या अगर शवयात्रा से तब सामना होता जब मैं पिता के साथ होता ? पिता ने अकेले क्यों भेजा मुझे, घर तक क्यों नहीं भेज गये, जिस दिन उन्हें कस्बे आना था तब तक गाँव में नहीं रख सकते थे ? घर पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं बताया उन्होंने ? रास्ते को क्या सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए कि वहाँ श्मशान पड़ता है ? ऐसे कई सवाल आज उठते हैं। यह भी दिखाई देता है कि जो पिता ने किया उसमें जीवन-शिक्षा थी, जिसे पिता के माध्यम से एक बुजुर्ग ने मुझे दी थी।
अँधेरा उतरने के पहले मैं घर पहुँच गया। पिता उस दिन क्या, आगे कुछ दिनों तक किसी तरह यह पुष्टि नहीं कर सकते थे कि मैं पहुँचा या नहीं, फोन तब कहाँ थे ! इतवार के लिए बीच में तीन दिन थे। इतने दिनों वे मुझे गाँव भी नहीं रोक सकते थे या रोकना ठीक नहीं समझते थे। मेरी पढ़ाई का हर्जा होता। पर अगले इतवार वे पक्के आये जो बीच-बीच में तीन इतवार तक गोल कर जाते थे। इसी में उनकी, मेरे पहुँचने को लेकर चिन्ता झलकी।
उस शाम मैंने अकेले चलना सीखा। सिर्फ अपने सहारे एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक पहुँचना, ऊबड़-खाबड़ डरावने रास्ते से गुजरना, शवयात्रा का सामना करना; जमीन के किस हिस्से पर पैर पड़ना है, वह खोजते हुए चलना।
सड़क पर स्कूल के लड़के ही लड़के बिछे थे। सब पालथी मारे बैठे, सिर सामने की ओर, जैसे आसन लगाये हों। मुझ जैसा कम उम्र का लड़का डर के मारे सिर नीचा कर लेता तो बगल वाला लड़का अपने हाथ से मेरा सिर उठाकर सामने की तरफ कर देता। मैं फिर नीचे देखने लगता-डामर की सड़क, काली चिकनाई पर जहाँ तहाँ उछले छोटे-छोटे कंकड़।
सवेरे एकाएक स्कूल की कक्षाएँ खाली होने लगी थीं। विद्यार्थियों को स्कूल के बाहर निकाला जा रहा था: स्कूल बन्द हो रहा था-यह सबको दिखता था लेकिन किस वजह से यह साफ-साफ किसी को पता नहीं था। बड़ी कक्षाओं के कुछ विद्यार्थी तूफान की तरह एक कक्षा में घुस जाते और फटकार लगाते-‘चलो, निकलो..बाहर चलो।’
फिर वे अपनी मुट्ठी ऊपर को उठाकर नारे लगाते-‘इन्किलाब जिन्दाबाद’ ‘भारत माता की जय’। उन नारों के बाद अध्यापक अपने आप ही पढ़ाना बन्द कर देते और कक्षा के बाहर चले जाते, उनके बाद लड़के। मिनटों में पूरा स्कूल गेट के बाहर था। वहाँ से हमें लाइनों में लगाकर कवायद कराते हुए पास ही कस्बे के मुख्य स्थान ड्यौढ़ी पर ले जाया गया। विद्यार्थियों की पंक्तियाँ जुलूस में तब्दील हो गयीं। ड्यौढ़ी पहुँचने पर नारे दुगुने जोर-शोर से चल निकले थे-‘इन्किलाब जिन्दाबाद’ भारत माता की जय, महात्मा गाँधी की जय, अँग्रेजों भारत छोड़ो, वन्दे मातरम्।’ तभी जाने कहाँ से एक लारी भरभराती आयी जिसमें से बूटधारी गोरे सिपाही फट-फट उतरे और जुलूस के सामने संगीनें तानकर खड़े हो गये। छात्र नेताओं ने नारे और तेज करवा दिये, फिर हमें वहीं बैठ जाने को कहा। लड़के आसन की मुद्रा में बैठ गये थे, गोलियाँ झेलने को तैयार।
मैं बार-बार नीचे देखने लगता था, क्योंकि तब मेरा डर कम हो जाता था, जमीन को देखने से बल मिलता था।
‘‘मुझे घर जाना..’’ मेरे मुँह से मुनमुनाहट निकल गयी।
‘‘चोप,’’ बगल वाले साथी ने घुड़क दिया, ‘‘बाहर निकलेगा तो वे भूनकर रख देंगे।’’
सामने चुस्त मुद्रा में सिपाही बन्दूकें ताने खड़े थे। कतार इस छोरे से उस छोर तक रस्सी की तरह खिंची हुई। घर जाने के लिए उन्हें पार करना होगा। मेरे भीतर जोर की धुकधुकी चालू हो गयी..पता नहीं कितनी बगल के साथी की घुड़क से, कितनी गोली मारे जाने के डर से। डर मरने का या गोली लगने पर जो दर्द होगा उसका-मैं नहीं जानता था। बस सामने जो संगीनें लिये आक्रामक मुद्रा में खड़े थे, उन्हें देखकर डर उठता था-वे हमें मारेंगे, हम पर झपट पड़ने को तैयार थे। हम उनके सामने प्याज की तरह लुढके पड़े थे। हमें बचानेवाले जो हो सकते थे वे भी सड़क पर बिछे थे। उसे रौंदते हुए सिपाही मुझ तक किसी भी क्षण आ सकते थे और फिर दे-मार-लात, घूँसे, उन संगीनों से भी। क्या वे मार डालेंगे मुझे ? मैं खत्म हो जाऊँगा इतनी जल्दी ? लोग तो बड़े होकर मरते हैं। मैं मर गया तो क्या होगा ? मेरे माँ-बाप रोएँगे। अरथी में मुझे बांधकर पहाड़ी के उसी रास्ते ले जाया जाएगा...क्या मेरे पिता मेरी अरथी के पीछे उसी तरह दौड़ेगे जैसे उस दिन वह व्यक्ति दौड़ता दिखा था-बदहवास, पागल-सा। तरह-तरह के ख्याल उठ रहे थे।
मैं इधर-उधर देख रहा था। बायीं तरफ एक दफ्तर की चारदीवारी पर मेहँदी की घनी बाड़ी थी। मन हुआ बन्दर की तरह उचकता उस तरफ निकल जाऊँ, बाड़ी के पीछे छिप जाऊँ, फिर वहाँ से गली में, जो उस इमारत और दूसरी दफ्तरी इमारत के बीच थी, सरपट दौड़ जाऊँ। तब मैं उस सड़क पर आ निकलूंगा। जो स्कूल से हमारे मुहल्ले को जाती थी, ड्यौढ़ी को दायीं तरफ छोड़ते हुए। सड़क पर एक बार पहुंच गया तो साधारण चाल में चलने लगूँगा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं कभी जुलूस में था। फिर वे मुझे क्यों पकड़ेंगे क्यों मारेंगे ?
‘‘मैं उधर से भाग जाऊँ ?’’ मैं बगल के लड़के से फिर फुसफुसाया। आँखों से मेहँदी की बाड़ की तरफ इशारा करते हुए।
‘‘डरपुक्का !’’ उसने नफरत-भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं फिर जमीन को देखने लगा।
तभी नारे फिर चल पड़े-‘इन्किलाब जिन्दाबाद, अँग्रेजो भारत छोड़ो।’
भाग जाने का मेरा ख्याल पता नहीं कहाँ उड़ गया। हिम्मत खुद में न भी हो तो बाहर से आ सकती है। उस लड़के में भी हिम्मत या तो जुलूस से आयी होगी या उस लक्ष्य से जिसके लिए वह लड़ाई थी। उस उम्र में लक्ष्य क्या समझ में आता होगा ! तो शायद भारत माता के प्रेम से उपजी हो। भारत के नाम से कुछ न उपजता हो, माता तो समझता ही होगा वह। मुझमें हिम्मत उससे आ गयी। अपने में हिम्मत पैदा करने का करिश्मा मेरे हाथ लग गया था। किसी में हिम्मत हो ही न–ऐसा तो शायद ही कभी होता हो, बात उसे जगाने की होती है-जैसे बाहर के दीये से अपने दीये का जला लेना ! उस समय मैं न केवल नारों के जवाब में मुट्ठी बांधने लगा, मेरी आवाज तेज हो गयी थीं, मुट्ठी वाला हाथ भी ऊपर जा रहा था।
नर्मदा एक छोटे से कुण्ड में प्रकट होती है। नीचे गिरते ही उसकी क्षीण धारा को एक धर्मकुण्ड में कैद कर लिया गया है जिसमें लोग पुण्य कमाने के नाम पर नहाते और गन्दगी मचाते हैं। जलाशय का पानी एक सड़क के नीचे से उतरकर एक तरफ निकलता है तो वे उसके इर्द-गिर्द शौच को बैठ जाते हैं, जैसे जहाँ नदी दिखाई दी कि गन्दा करने के लिए झपट पड़े हमारे भक्त, तीर्थयात्री, नगरवासी, भारतवासी। बेचारी नदी नाली की तरह किसी तरह आगे चली तो नगरियों ने उसे फौरन एक छोटे बाँध में बाँध तालाब बना लिया-मुँह धोने, खँखारने कपड़े धोने और नौका विहार कराकर पैसा कमाने के लिए। नर्मदा अपने को किसी तरह छुड़ा कीचड़वाली नाली की शक्ल में आगे खचुरती, अपने जल को कीचड़ के ऊपर धीरे-धीरे बहाती आगे बढ़ती है। फिर प्रवाह तेज होने लगता है, जैसे जान बचाकर आदमी की बस्ती से दूर भाग जाना चाहती हो। बस्ती के बाहर पहुँचते ही वह कपिलधारा बनकर खूब नीचे, खाई में पत्थरों के ऊपर गिरती है...अपने को तोड़ते हुए, गन्दगी को निकालते, स्वयं को निथारते हुए। यहाँ से दोनों तरफ पहाड़ की सुरक्षा है-आगे, काफी दूर तक। अब जहाँ तक हो सकेगा वह आदमी की बस्ती से दूर-दूर चलना चाहेगी, ताकि खुद को शुद्ध रख सके, उसे अपने से ही दुर्गन्ध न आने लगे, लेकिन यह शातिर चीज आदमी, जहाँ नर्मदा होगी, वहाँ पहुँच जाएगा, घर बैठा लेगा, बस्ती जमा लेगा, गन्दगी फैलाएगा...कहेगा कि उसके धर्मतीर्थ हैं, जबकि देखो तो धर्म तुममें कहाँ, नर्मदा में है। नर्मदा से तुम्हें अपने में उतारना है। पर तुम तो उसी को नष्ट करने पर तुले हुए हो। नर्मदा और भारतीय नारी में कितनी समानता है।
नर्मदा ने शुरूआत में ही एक सीख ले ली, कपिलधारा बनते ही-जब-जब तुममें गन्दगी इकट्ठा हो जाए, पहाड़-पत्थरों पर खुद को दे मारो, स्वयं को पछीटते चलो, रेशा-रेशा, कण-कण। इसी तरह तुम खुद को साफ रख सकते हो। नर्मदा की यात्रा कैद से निकलकर बहने, प्रपात बनकर गिरने, फिर बहने की है। जहाँ कूड़ा-कचरा, दिखावा-पाखण्ड, नोचना-खसोटना हुआ वहाँ उथली होकर ऊपर-ऊपर से निकल जाओ, जहाँ स्वच्छता प्रेम पाओ वहाँ रम जाओ, गहरी हो जाओ, धीरे-धीरे बहो...।
सोन नद चतुर है, कुण्ड से निकलते ही भागने लगता है, ढलानों में इधर से, उधर से..इतनी पतली धारा में कि दिखाई भी न दे..और मुश्किल से सौ गज आगे जाकर नीचे कूद जाता है, कूदकर तिरोहित हो जाता है, फिर आसानी से पकड़ में नहीं आता। पुरुष है !
मुझे नर्मदा की कहानी सृजन की कहानी भी लगती है-लिखना माने अपने को बचाये रखने, शुद्ध करने के क्रम में निरन्तर स्वयं को तोड़ते चलना, तरह-तरह से बहना। रचनाओं-प्रपातों में गिरने से प्राणवायु निर्मित होती है, जो स्वयं को तो जीवित रखती ही है, वातावरण में भी बिखरती है। मनुष्य जाति, समाज की गन्दगी न भी धुल पाये तो कुछ के अन्तर्मन तो निर्मल हुए, आसपास का वातावरण तो शुद्ध हुआ। जरूरत हुई तो नर्मदा विध्वंसकारी रूप भी धारण करती है।
जो सृजन का सच है वही क्या जीवन का सच भी नहीं ? धरती पर हमारे आते ही समाज की गन्दगी, उसकी जंग लगी संस्थाएँ, रूढ़ियाँ जड़ विचार हमें अपने आगोश में लेने को दौड़ते हैं, हमें नष्ट कर देने को आतुर। भयभीत हम भागते हैं खुद को बचाने के लिए। बच सके यही क्या कम है ! खुद को, अपने आसपास के लोगों को जीने में आस्था दे सके तो यह उसका कितना अच्छा प्रतिदान हुआ, जिसे कुछ लोग अपने जीवन की तमाम विषम परिस्थितियों के बीच, अपने जीवन संघर्ष के साथ-साथ हमारे लिए कर गये-अनायास। वे जो हमारे सामने जीवित थे, उनके प्रति हम अपने अनुग्रह को ठीक से प्रकट भी नहीं कर सके थे। हम वह नहीं कर पाये तो यह तो कर सकते हैं कि उन लोगों की स्मृति को अपने जीवन में लौटा-लौटा कर लाएँ, उनकी सुगन्ध को बाहर बिखेंरे।
मुझमें कितना मेरा अपना है ? जो है वह भी मेरा कहाँ ! कहीं से आया होगा, जिसे मैंने तराश कर वह बनाया, जिसे आज अपना कहता हूँ। इस पोटली को कलेजे से लगाये चल रहा हूँ। चल रहा हूँ या कि भाग रहा हूँ ? तेजी से बीत तो रहा ही हूँ। मेरी यात्रा समाप्ति की ओर है, लेकिन नर्मदा समाप्त नहीं होती, सागर में समा जाती है। और उसका चलना, बहना भी अनवरत है-जाती हुई जलधारा के पीछे आती असंख्य जलधाराएँ, एक-पर-एक। क्या ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है या कि मेरा चलना-बहना मेरे जीवन के साथ ही समाप्त हो जाएगा ? वह अनवरत हो सकता है अगर उसमें उनका बहना समाहित हो जाए जो मेरे आगे गये, जो मेरे पीछे बहेंगे..अनवरत बहती मानव जलधारा !
मनुष्य को यह सिफत मिली है कि जो पीछे छूट गया वह उसे देख सकता है..काफी कुछ। बीत हुए का सत्त्व निकाल सकता है। अपने चलने-बहने को कोई उसी वक्त देखता चल सकता है क्या ? शायद हाँ, कोशिश करके...थोड़ा-बहुत। जो वह जी रहा है उसके परे कितना कुछ है वह भी दिख सकता है-विलक्षण क्षणों में। अपनी और अपनों की जीवन कहानियाँ कह, उनके तनावों-द्वन्द्वों का खुलासा कर वह असंख्य जलधाराओं की सृष्टि कर सकता है जिनके आलोक में आने वाले लोग भी अपना बहना देख सकें।
नीम की डगाल से लटका मूँज की डोरियों का बना एक छींका, जिस पर रखी थी रसखीर, लाल रंग मिट्टी की चपिया में, ढकना भी मिट्टी का। शाम पिता ने अपने आठ साल के लड़के के लिए गन्ने का रस मँगाया था और कण्डों के ऊपर रोटी-दाल के बाद मिट्टी की इस चपिया में खुद खीर पकायी थी। रात के खाने के बाद जो बची उसे उन्होंने छींके पर टाँग दिया था, बिल्ली से बचे और रात भर चाँदनी की ठण्डक चपिया में पहमती भी रहे।
गोल-गोल बड़े चबूतरे पर नीम का वह पेड़ खासा बड़ा और छायादार था। दिन में वहाँ उस गाँव की एकमात्र प्राथमिक पाठशाला लगती जिसमें पिता अकेले शिक्षक थे। रात को उसी चबूतरे पर दो खटियाँ बिछी थी। चाँदनी की छोटी-बड़ी बुन्दकियाँ चबूतरे पर फैली थीं। ऊपर नीम की पत्तियाँ हल्के-हल्के डोलतीं, पत्तियों के पार तारे टिमटिमाते थे। तारों में मैं सप्तर्षि खोजता रहा। दिखाई दिये तो मैंने गिने-पूरे सात। फिर नजर डगाल से लटके छींके पर अटक गयी-रसखीर..आसमान और जमीन के बीच। मेरा ध्यान उसी में था, विश्वास भी था कि कल मिलेगी। यह समझ नहीं थी कि खीर तो कल खत्म भी हो जाएगी, पेड़ के ऊपर तारे..वे कभी न मिलेंगे, पर बराबर रहेंगे।
थोड़ी दूर पर पिता की चारपाई थी। बीच में पानी का एक घैला और एक लुटिया। नीम का यह पेड़ ही पिता का घर था। जाड़े-बरसात में वे स्कूल की जो एकमात्र कोठरिया थी, वहाँ चले जाते। कोठरिया में एक किनारे एक टूटी-सी लकड़ी की सन्दूकची में रखी उनकी पूरी गृहस्थी-दो धोती, एक लाल गमछा, दो कुर्ते, आटा-दाल की कुछ मोटी-मोटी कन्सरियाँ, कुछ डिब्बे। सन्दूकची के ऊपर रखा रहता एक छोटा-सा पीतल का सिंहासन, जिसके ऊपर चाँदी का एक छोटा छत्र था। सिंहासन में दो छोटे-छोटे शालिग्राम के बीच एक छोटे से बालमुकुन्द जिनके नाक-नक्श मुश्किल से दिखाई देते थे।
चबूतरे के नीचे गाँव की बड़ी गली थी जो बाहर से गाँव में आती थी और गाँव के बाहर निकलती थी। नींद आने तक वहाँ से जब-तब उठती चमरौधों की चर्म-मर्र सुनाई देती रही।
अगली सुबह कण्डों पर ही पिता ने खाना बना दिया-मूँग की दाल, रोटी और कण्डों की बुझती आग में भुने हुए आलू जिन्हें छिलके समेत मीस, नमक-मिर्च-प्याज मिला भरता बना लिया गया। सबसे बाद में रसखीर जो चाँदनी पीकर अमृत हो गयी थी।
पिता मुझसे मतलब की ही बात बोलते थे। मैं अब सोच सकता हूँ कि अपने बारे में वे जानते थे कि उनकी जुबान कर्कश थी, कड़वे बोल मुझ तक नहीं पहुँचाना चाहते थे, खासतौर से तब, जब वे मुझे कस्बे से अपने गाँव एक दिन के लिए लाये थे-इसको लेकर वे सजग थे। वे गाँव में पढ़ाते थे, माँ कस्बे में। मैं कस्बे के स्कूल में पढ़ता था। पिता इतवार के इतवार कस्बे आते थे, कभी-कभी नहीं भी आते थे।
दस बजे से पाठशाला लग गयी। लड़के (लड़कियाँ नहीं थीं) मैली-कुचैली पोशाक में, कोई-कोई कमीज से नाक पोंछते, सब पाटी बोरका के साथ चबूतरे पर फैल गये। रात चबूतरे पर चाँदनी की नीरवता और शीतलता थी, अब जैसे सुबह के पक्षियों का कलरव और गर्मी। पिता ने मेरे लिए दो-चार लड़कों को पहाड़े लिखवाने और जाँचने का काम सौंप मुझे थोड़ी देर का छोटा-मोटा मास्टर बना दिया। दोपहर के थोड़ा बाद छुट्टी कर दी गयी और पिता मुझे कस्बे वापस भेजने चल दिये। चलने से पहले उन्होंने फिर खाने को दिया-सवेरे की बची रोटियाँ, भुने आलुओं का भर्ता। उनका सिद्धांत था-कहीं जाने के पहले पेट जरूर भर लो, वर्ना चलोगे कैसे और पता नहीं खाना कब और कहां मिले। खाने के बाद हमने भरपेट पानी पिया और निकल पड़े।
बैलगाड़ी वाले रास्ते के किनारे-किनारे पिता चले जा रहे थे। मैं उनसे हमेशा पीछे रह जाता, फिर उनकी बराबरी पर आ जाने के लिए दौड़ता। पीछे से दिखाई देती थीं धोती के नीचे खुलती उनकी टाँगें-दुबली पर सुडौल बराबर चलती टाँगें..जो न तेज होती थीं, न पिछड़ती थीं, चलती चली जाती थीं, चलती चली जाती थीं। रास्ते में एक कुएँ पर रुककर उन्होंने झोले से लोटा-डोर निकाली। कुएँ से लोटे में पानी निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने एक हाथ की चुल्लू बनायी, एक हाथ से लोटे का पानी उसमें डालता गया, पीता गया। मीठा पानी ठण्डा पृथ्वी के गर्भ से खास मेरे लिए निकला पानी। साफ, ऊर्जा भर देने वाला सिर्फ उतना जितनी मुझे जरूरत थी।
पिता आधे रास्ते तक पहुँचा गये। उसके आगे का रास्ता मुझे ठीक से समझा दिया-‘बैलगाड़ी के इसी रास्ते को पकड़े रहना, जब एक बड़ा बगरद का पेड़ मिले तो बायें मुड़ जाना। एक मोटी पगडण्डी होगी वह, जो सीधे पहाड़ी की जड़ तक ले जाएगी। फिर पहाड़ी की सीढ़ियाँ पकड़ लेना, सीढ़ियाँ पहले ऊपर चढ़ेंगी हरी तलैया तक, फिर उतरेंगी। उतरते ही अपनी बस्ती आ जाएगी।’ उसके बाद मैं आगे की तरफ चला वे वापस उस गाँव की ओर लौट पड़े जहाँ से हम चले थे।
मैं पीछे मुड़-मुड़कर पिता को गाँव लौटते देखता रहा। धोती के नीचे झलकती उनकी टाँगों को भी। उन्होंने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, या शायद देखा हो जब मैंने न देखा हो।
पहाड़ की जड़ तक मैं तेज चला, पहाड़ की सीढ़ियों पर हाँफते हुए। सीढ़ियों की चढ़ाई जहाँ खत्म हुई वहाँ हरी तलैया मिली। पानी के ऊपर उतराती हरी काई, नीचे पानी भी हरा। तलैया पर चारों तरफ से घिरी पहाड़ियों की हरियाली का अक्स पड़ता था, शायद इसलिए पानी हरा दिखता था। मैं तलैया की पट्टी पर थोड़ी देर सुस्ताने बैठा। सामने सीढ़ियों पर कपड़े फींचती एक औरत, काई हटाकर डुबकी मारता एक बूढ़ा आदमी, ऊपर वाली सीढ़ी से कूदते, तैरकर घाट तक वापस आते दो-तीन मेरी उम्र के बच्चे। इस तरफ के घाट पर आठ-दस आदमी डुबकी लगाकर एक-एक कर बाहर निकल रहे थे, निकलकर भीगे कपड़े पहनते हुए।
वहाँ से रास्ता थोड़ी दूर तक बड़े पत्थरों पर से चला, फिर छोटे सपाट पत्थरों पर से नीचे लुढ़कने लगा। चलने वाला मैं अकेला। तभी सामने से कुछ, लोग मेरी तरफ आते दिखे। ‘राम नाम सत्य है’ की मिली-जुली मद्धिम आवाज-जितनी एकरस, उतनी ही डरावनी। चार-छः लोग एक अरथी को उठाए थे। नीचे उठंग धोती, ऊपर नंगा बदन, सिर या कन्धों पर लाल गमछा। मैं डरकर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। दस-पन्द्रह लोगों की वह छोटी-सी टुकड़ी ‘राम नाम सत्य’ करती ज्यों-ज्यों मेरे पास आती जा रही थी, मेरी धुकधुकी बढ़ती जाती थी। जब वह मेरे बगल से गुजरी तो मेरे चारों तरफ डर का घटाटोप-ऊपर सूना आसमान, नीचे उतरती शाम की छाया, चारों तरफ पहाड़, बीच के रास्ते में बड़े-बड़े पत्थर, जिन पर से गुजरती वह शवयात्रा और एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा मैं।
कहां जा रहे थे ये लोग, किसको ऊपर बांधे ? उन सबके चेहरे, स्वर चाल सब एक तरह के और संजीदा क्यों थे। मैं सोच रहा था।
लोग मरते हैं यह तो मैं जानता था लेकिन यह नहीं जानता था कि क्यों मरते हैं। लोगों की टोली निकल गयी। मैं सपाट पत्थरोंवाले रास्ते पर आ गया तो सामने से एक वृद्धावस्था को छूता आदमी, उघारे बदन, रोता-बिलखता दौड़ता चला आ रहा था। उसके आँसू और आवाज दोनों सूख गये थे। चेहरे पर ऐसी वेदना, ऐसी असहायता-जैसे उसका सबकुछ लुट गया हो। आधा पागल, बदहवास वह अरथी के पीछे दौड़ा चला जा रहा था जैसे भैंस दौड़ती है, जब उसके छोटे मरे बच्चे को उठाकर ले जाते हैं।
वह पहली शवयात्रा थी जो मैंने देखी, अकेले। इसके पहले घर के बाहर से गुजरती कई शवयात्राओं की झलक दिखी थी, माँ दौड़कर किवाड़ बन्द कर लेती थीं। पिता ने मुझे उस रास्ते से भेजा जहाँ पास में श्मशान था, हरी तलैया थी जहाँ शवयात्रा से लौटकर लोग नहाते थे।
कुछ फर्क पड़ता क्या अगर शवयात्रा से तब सामना होता जब मैं पिता के साथ होता ? पिता ने अकेले क्यों भेजा मुझे, घर तक क्यों नहीं भेज गये, जिस दिन उन्हें कस्बे आना था तब तक गाँव में नहीं रख सकते थे ? घर पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं बताया उन्होंने ? रास्ते को क्या सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए कि वहाँ श्मशान पड़ता है ? ऐसे कई सवाल आज उठते हैं। यह भी दिखाई देता है कि जो पिता ने किया उसमें जीवन-शिक्षा थी, जिसे पिता के माध्यम से एक बुजुर्ग ने मुझे दी थी।
अँधेरा उतरने के पहले मैं घर पहुँच गया। पिता उस दिन क्या, आगे कुछ दिनों तक किसी तरह यह पुष्टि नहीं कर सकते थे कि मैं पहुँचा या नहीं, फोन तब कहाँ थे ! इतवार के लिए बीच में तीन दिन थे। इतने दिनों वे मुझे गाँव भी नहीं रोक सकते थे या रोकना ठीक नहीं समझते थे। मेरी पढ़ाई का हर्जा होता। पर अगले इतवार वे पक्के आये जो बीच-बीच में तीन इतवार तक गोल कर जाते थे। इसी में उनकी, मेरे पहुँचने को लेकर चिन्ता झलकी।
उस शाम मैंने अकेले चलना सीखा। सिर्फ अपने सहारे एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक पहुँचना, ऊबड़-खाबड़ डरावने रास्ते से गुजरना, शवयात्रा का सामना करना; जमीन के किस हिस्से पर पैर पड़ना है, वह खोजते हुए चलना।
सड़क पर स्कूल के लड़के ही लड़के बिछे थे। सब पालथी मारे बैठे, सिर सामने की ओर, जैसे आसन लगाये हों। मुझ जैसा कम उम्र का लड़का डर के मारे सिर नीचा कर लेता तो बगल वाला लड़का अपने हाथ से मेरा सिर उठाकर सामने की तरफ कर देता। मैं फिर नीचे देखने लगता-डामर की सड़क, काली चिकनाई पर जहाँ तहाँ उछले छोटे-छोटे कंकड़।
सवेरे एकाएक स्कूल की कक्षाएँ खाली होने लगी थीं। विद्यार्थियों को स्कूल के बाहर निकाला जा रहा था: स्कूल बन्द हो रहा था-यह सबको दिखता था लेकिन किस वजह से यह साफ-साफ किसी को पता नहीं था। बड़ी कक्षाओं के कुछ विद्यार्थी तूफान की तरह एक कक्षा में घुस जाते और फटकार लगाते-‘चलो, निकलो..बाहर चलो।’
फिर वे अपनी मुट्ठी ऊपर को उठाकर नारे लगाते-‘इन्किलाब जिन्दाबाद’ ‘भारत माता की जय’। उन नारों के बाद अध्यापक अपने आप ही पढ़ाना बन्द कर देते और कक्षा के बाहर चले जाते, उनके बाद लड़के। मिनटों में पूरा स्कूल गेट के बाहर था। वहाँ से हमें लाइनों में लगाकर कवायद कराते हुए पास ही कस्बे के मुख्य स्थान ड्यौढ़ी पर ले जाया गया। विद्यार्थियों की पंक्तियाँ जुलूस में तब्दील हो गयीं। ड्यौढ़ी पहुँचने पर नारे दुगुने जोर-शोर से चल निकले थे-‘इन्किलाब जिन्दाबाद’ भारत माता की जय, महात्मा गाँधी की जय, अँग्रेजों भारत छोड़ो, वन्दे मातरम्।’ तभी जाने कहाँ से एक लारी भरभराती आयी जिसमें से बूटधारी गोरे सिपाही फट-फट उतरे और जुलूस के सामने संगीनें तानकर खड़े हो गये। छात्र नेताओं ने नारे और तेज करवा दिये, फिर हमें वहीं बैठ जाने को कहा। लड़के आसन की मुद्रा में बैठ गये थे, गोलियाँ झेलने को तैयार।
मैं बार-बार नीचे देखने लगता था, क्योंकि तब मेरा डर कम हो जाता था, जमीन को देखने से बल मिलता था।
‘‘मुझे घर जाना..’’ मेरे मुँह से मुनमुनाहट निकल गयी।
‘‘चोप,’’ बगल वाले साथी ने घुड़क दिया, ‘‘बाहर निकलेगा तो वे भूनकर रख देंगे।’’
सामने चुस्त मुद्रा में सिपाही बन्दूकें ताने खड़े थे। कतार इस छोरे से उस छोर तक रस्सी की तरह खिंची हुई। घर जाने के लिए उन्हें पार करना होगा। मेरे भीतर जोर की धुकधुकी चालू हो गयी..पता नहीं कितनी बगल के साथी की घुड़क से, कितनी गोली मारे जाने के डर से। डर मरने का या गोली लगने पर जो दर्द होगा उसका-मैं नहीं जानता था। बस सामने जो संगीनें लिये आक्रामक मुद्रा में खड़े थे, उन्हें देखकर डर उठता था-वे हमें मारेंगे, हम पर झपट पड़ने को तैयार थे। हम उनके सामने प्याज की तरह लुढके पड़े थे। हमें बचानेवाले जो हो सकते थे वे भी सड़क पर बिछे थे। उसे रौंदते हुए सिपाही मुझ तक किसी भी क्षण आ सकते थे और फिर दे-मार-लात, घूँसे, उन संगीनों से भी। क्या वे मार डालेंगे मुझे ? मैं खत्म हो जाऊँगा इतनी जल्दी ? लोग तो बड़े होकर मरते हैं। मैं मर गया तो क्या होगा ? मेरे माँ-बाप रोएँगे। अरथी में मुझे बांधकर पहाड़ी के उसी रास्ते ले जाया जाएगा...क्या मेरे पिता मेरी अरथी के पीछे उसी तरह दौड़ेगे जैसे उस दिन वह व्यक्ति दौड़ता दिखा था-बदहवास, पागल-सा। तरह-तरह के ख्याल उठ रहे थे।
मैं इधर-उधर देख रहा था। बायीं तरफ एक दफ्तर की चारदीवारी पर मेहँदी की घनी बाड़ी थी। मन हुआ बन्दर की तरह उचकता उस तरफ निकल जाऊँ, बाड़ी के पीछे छिप जाऊँ, फिर वहाँ से गली में, जो उस इमारत और दूसरी दफ्तरी इमारत के बीच थी, सरपट दौड़ जाऊँ। तब मैं उस सड़क पर आ निकलूंगा। जो स्कूल से हमारे मुहल्ले को जाती थी, ड्यौढ़ी को दायीं तरफ छोड़ते हुए। सड़क पर एक बार पहुंच गया तो साधारण चाल में चलने लगूँगा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं कभी जुलूस में था। फिर वे मुझे क्यों पकड़ेंगे क्यों मारेंगे ?
‘‘मैं उधर से भाग जाऊँ ?’’ मैं बगल के लड़के से फिर फुसफुसाया। आँखों से मेहँदी की बाड़ की तरफ इशारा करते हुए।
‘‘डरपुक्का !’’ उसने नफरत-भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं फिर जमीन को देखने लगा।
तभी नारे फिर चल पड़े-‘इन्किलाब जिन्दाबाद, अँग्रेजो भारत छोड़ो।’
भाग जाने का मेरा ख्याल पता नहीं कहाँ उड़ गया। हिम्मत खुद में न भी हो तो बाहर से आ सकती है। उस लड़के में भी हिम्मत या तो जुलूस से आयी होगी या उस लक्ष्य से जिसके लिए वह लड़ाई थी। उस उम्र में लक्ष्य क्या समझ में आता होगा ! तो शायद भारत माता के प्रेम से उपजी हो। भारत के नाम से कुछ न उपजता हो, माता तो समझता ही होगा वह। मुझमें हिम्मत उससे आ गयी। अपने में हिम्मत पैदा करने का करिश्मा मेरे हाथ लग गया था। किसी में हिम्मत हो ही न–ऐसा तो शायद ही कभी होता हो, बात उसे जगाने की होती है-जैसे बाहर के दीये से अपने दीये का जला लेना ! उस समय मैं न केवल नारों के जवाब में मुट्ठी बांधने लगा, मेरी आवाज तेज हो गयी थीं, मुट्ठी वाला हाथ भी ऊपर जा रहा था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book