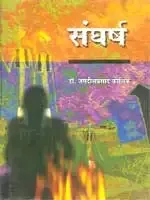|
पौराणिक >> संघर्ष संघर्षजगदीशप्रसाद कौशिक
|
418 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत उपन्यास वैदिकोत्तर संस्कृति तथा तात्कालिक सामाजिक और धार्मिक परिवेश को अपने में समाविष्ट किये हुए है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रस्तुत उपन्यास लेखक का कथा-साहित्य में सफल प्रयास है। यद्यपि लेखक
भाषा-विज्ञान और काव्यशास्त्र के प्रतिष्ठित विद्वान हैं तदपि सर्जनात्मक
साहित्य में प्रकाशन की दृष्टि से यह उत्तम कृति है।
प्रस्तुत उपन्यास वैदिकोत्तर संस्कृति तथा तात्कालिक सामाजिक और धार्मिक परिवेश को अपने में समाविष्ट किये हुए है। लेखक ने भारतीय परिवेश को नवीन दृष्टि से परखा और उसे यथार्थवादी रूप प्रदान करने का स्तुत्य प्रयास किया है। पूर्व उपन्यास में देवों का आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत न कर उन्हें सजीव प्राणियों के परिधान में देखा है जिससे उनके गुणावगुणों पर निष्पक्ष दृष्टिपात किया जा सके। यही स्थिति असुरों की है। असुरों को देवों का भाई माना गया है। इस प्रकार तत्कालीन प्रचलित इन दो संस्कृतियों की गतिविधियों का सम्यक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है तथा इन संस्कृतियों का पारस्परिक राग-द्वेषों के परिणाम स्वरूप मानव-संस्कृति के उन्मेष एवं विकास को अत्यन्त मनोहारी एवं साहित्यिक शैली में दिग्दर्शित किया गया है।
लेखक की मान्यता है कि वैवस्वत मनु ने मानव-संस्कृति की स्थापना एवं सुदृढ़ एवं परिपक्व आधारों पर की है जो चिरस्थायी हैं आपने सक्षम और अमर-विधि-नियमों की व्यवस्था की जो मानव-संस्कृति को विघटित अथवा विस्थापित होने से रोकती रही हैं और आज भी नव-दुल्हन की भाँति सजी-धजी एवं आकर्षक बनी हुई जीवित हैं, अमर हैं।
यह उपन्यास समय की गति के अनुरूप मानव के चिंतन ओर सोच को साकार करने में सफल हुआ है। लेखक के कथन से यह ध्वनित होता है कि अति नियंत्रण प्रगति का बाधक होता है। इसलिए संस्कृतियों के विकास में लचीलापन होना उसका गुण होता है, दोष नहीं।
प्रस्तुत उपन्यास वैदिकोत्तर संस्कृति तथा तात्कालिक सामाजिक और धार्मिक परिवेश को अपने में समाविष्ट किये हुए है। लेखक ने भारतीय परिवेश को नवीन दृष्टि से परखा और उसे यथार्थवादी रूप प्रदान करने का स्तुत्य प्रयास किया है। पूर्व उपन्यास में देवों का आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत न कर उन्हें सजीव प्राणियों के परिधान में देखा है जिससे उनके गुणावगुणों पर निष्पक्ष दृष्टिपात किया जा सके। यही स्थिति असुरों की है। असुरों को देवों का भाई माना गया है। इस प्रकार तत्कालीन प्रचलित इन दो संस्कृतियों की गतिविधियों का सम्यक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है तथा इन संस्कृतियों का पारस्परिक राग-द्वेषों के परिणाम स्वरूप मानव-संस्कृति के उन्मेष एवं विकास को अत्यन्त मनोहारी एवं साहित्यिक शैली में दिग्दर्शित किया गया है।
लेखक की मान्यता है कि वैवस्वत मनु ने मानव-संस्कृति की स्थापना एवं सुदृढ़ एवं परिपक्व आधारों पर की है जो चिरस्थायी हैं आपने सक्षम और अमर-विधि-नियमों की व्यवस्था की जो मानव-संस्कृति को विघटित अथवा विस्थापित होने से रोकती रही हैं और आज भी नव-दुल्हन की भाँति सजी-धजी एवं आकर्षक बनी हुई जीवित हैं, अमर हैं।
यह उपन्यास समय की गति के अनुरूप मानव के चिंतन ओर सोच को साकार करने में सफल हुआ है। लेखक के कथन से यह ध्वनित होता है कि अति नियंत्रण प्रगति का बाधक होता है। इसलिए संस्कृतियों के विकास में लचीलापन होना उसका गुण होता है, दोष नहीं।
पुरोवाक्
प्राणि-समुदाय के दो प्रमुख तत्त्व होते हैं। भौतिक उन्नति का आविर्भाव
सभ्यता कहलाता है और सभ्यता का देदीप्यमान सूक्ष्म स्वरूप संस्कृति कहलाती
है। प्रत्येक जाति या सम्प्रदाय की अपनी-अपनी संस्कृति होती है। संस्कृति
उस जाति या समुदाय की पहचान होती है। जिसे हम भारतीय या आर्यसंस्कृति कहते
हैं तो उससे भरतखण्ड को संकेतित किया जाता है। वेद, उपनिषद्, ब्राह्मण
ग्रंथ, आरण्यक आदि ग्रंथों की दीप्ति, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ,
विश्वामित्र, गुत्समद, याज्ञवल्कय, जैसे मेधावी ऋषियों की जाज्वल्यमान्
आकृति तथा मनु, ययाति, मांधाता, रघु, नहुष जैसे तेजस्वी एवं प्रतापी
राजाओं का शौर्य नयनों के समक्ष आ उपस्थित होता है। इन्हीं की विचार सरणि
और कार्य-कलापों की सूक्ष्म-गरिमा ही भारत की प्राचीन संस्कृति के नाम से
अभिहित की जाती है। मैक्समूलर जैसे पाश्चात्य विद्वान इस काल को
आर्य-संस्कृति का मध्याह्न काल कहते हैं। इनके अनुसार वैदिक युग आर्यों की
अप्रतिम उन्नति का काल था। इस संस्कृति का बीजवपन बहुत ही पहले ही हो चुका
था।
इसी विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने भारतीय संस्कृति के अध्ययन और मनन का निश्चय किया। पाश्चात्य जर्मन विद्वान का कथन किसी सीमा तक सत्य प्रतीत होता है। कोई भी मानव-समुदाय अपने प्रारम्भिक काल में इतने उच्च विचार और सूक्ष्म अभिव्यक्ति में सक्षम नहीं हो सकता। इस विचार को ही आधार मानकर मैंने देव-संस्कृति और असुर-संस्कृति को काल्पनिक या अति आध्यात्मिक न मानकर विशुद्ध सांसारिक परिप्रेक्ष्य में देखा है। इन संस्कृतियों में मैंने उन त्रुटियों को दृष्टिगत किया जो किसी समुदाय की प्रारंभिक त्रुटियाँ होती हैं। मस्तीभरा जीवन, उपभोग्या नारी का स्वरूप, सोमरस का देवों द्वारा और सुरा का असुरों द्वारा पान, अनेक स्त्रियों के साथ अवैध संबंध आदि।
मैं यह मानकर चलता हूँ कि इन्हीं संस्कृतियों की त्रुटियों का निराकरण करते हुए महान् चिंतक एवं सिद्धांतनिष्ठ व्यक्तित्व के धनी परमश्रद्धेय वैवस्वत मनु के मन मानव-संस्कृति की स्थापना का श्रीगणेश किया। यदि मैं कहूँ कि मानव-संस्कृति देव-संस्कृति की त्रुटियों का ही संशोधित संस्करण है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रसिद्ध शायर इकबाल ने ठीक ही कहा है कि विश्व की बड़ी संस्कृतियाँ जहाँ से मिट गयीं, किन्तु इस संस्कृति में कुछ है कि आज भी जीवित है। इसी विचारधारा की अमिट छाप मेरे हृदयस्थल पर पड़ी है और मुझमें इस संस्कृति को जाँचने और परखने की बलवती इच्छा ने जनम लिया। इसी इच्छा का परिणाम ही इन दो पुस्तकों-महा अभियान एवं संघर्ष-का प्रणयन है। इस संस्कृति में बहुत उतार-चढ़ाव और संकट आये किन्तु यह अटूट और अजस्र गति से आज तक प्रवाहमान है।
मैं शरीर-विज्ञान का छात्र तो नहीं रहा किन्तु इस क्षेत्र में सोचने और विचारने का अधिकार तो मुझे प्रकृतिदत्त है। मैं अब यह और अधिक शक्ति के साथ मानने के लिये बाध्य हूँ कि हमारे रक्त में अपनों से, केवल अपनों से विद्रोह करने की क्षमता पुराकाल से ही चली आ रही है। इसका कारण तो मैं नहीं जानता किन्तु इतना अवश्य है कि इस संस्कृति में आदिकाल से ही इसके प्रति विद्रोह का भाव अनवरत गति से चला आ रहा है। महर्षि अत्रि ने वैवस्वत मनु के साथ इस मानव-संस्कृति की स्थापना की और उनके शिष्य ऋषि उतथ्य ने इसकी जड़ों को शक्तिशाली और बलवती बनाने का अदम्य प्रयास किया तब भी इसके विरोध के लिये विरोध हुआ। पुलस्त्य और विश्रवा ने अपनी पूर्ण शक्ति से मानव-संस्कृति का विरोध किया और रक्ष-संस्कृति की स्थापना की। इसका हमारा पुराण साहित्य साक्षी है। यही रक्ष-संस्कृति आगे चलकर आर्यों के लिये अत्यन्त बाधक सिद्ध हुई।
इस उपन्यास में मैंने इसी समय की मानव-संस्कृति को समुपस्थित करने का प्रयास किया है। इस समय के प्रमुख स्तम्भ थे, दक्षिण के यादव नरेश हैहयवंशी सह्स्रार्जुन, उत्तर के कान्यकुब्ज नरेश भरतवंशी गाधि और बाद में उनके पुत्र विश्वरथ, मध्यप्रदेश अयोध्या के नरेश अज, कौशल के नरेश तथा मिथिला नरेश निमि अथवा जनक। इन प्रमुख नरेशों के अतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे संघ-राज्यों का उदय भी आर्यावर्त की भूमि पर हो चुका था। उधर दूसरी ओर उच्च विचारधारा के उद्बोधक चिंतनशील मनीषियों ने भी इस पुण्य भूमि पर अवतरण किया, ये थे-अत्रि, वसिष्ठ, गृत्समद, अगस्त्य, विश्वामित्र, जाबाली, कपिल, याज्ञवल्कय, ऐतरेय, कणाद् आदि। स्त्री ऋषिकाओं में मदालसा, अपाला, लोपामुद्रा, अनसूया आदि।
साथ ही रक्ष-संस्कृति के अपूर्व योद्धा रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, विभीषण, मूल्यावन् आदि ने रक्ष-संस्कृति के प्रसार एवं प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और अभूतपूर्व वैज्ञानिक उन्नति का परिचय दिया। यक्षों में कुबेर को नहीं भुलाया जा सकता है। इतना सब होने पर भी सजग ऋषियों ने आर्य समाज में अंदर पनप रहे पारस्परिक वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष को आर्यों के सजग मनीषियों ने तुरंत चिह्नित कर लिया। राजाओं में पनप रहे सम्प्रभुता की भावना और एकांत भक्ति का धुव्रीकरण करने की कुत्सित भावना और फलस्वरूप ब्राह्मण में उत्पन्न पीड़ा हीनभावना को पहचाना और चिंतित हो उठे। ब्राह्मण युवकों में समुद्भूत विद्रोह के भाव, क्षत्रिय राजकुमारों के लिए और क्षत्रिय कुमारों में एवं राजाओं में ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या भाव तीव्रगति से उमड़ने लगा था चिंतनशील मनीषी ऋषियों को आर्यावर्त की संस्कृति के पैर डगमगाते दृष्टिगत होने लगे तथा सुसंगठित आर्य-संस्कृति के विघटन के चिह्न भी दिखाई देने लगे और इन दुष्प्रवृत्तियों के निराकरण के उपाय उपनिषदों और आरण्यकों के माध्यम से किये जाने के प्रयास प्रारंभ हो गये।
पुरा उत्तर कालीन संस्कृति के इसी रूप को प्रस्तुत उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया गया है। भारतीय समाज को सुदृढ़ता प्रदान करने के गौरवमय प्रयास को ऋषियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही भारतीय समाज में नारी की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। सुशिक्षिता तथा चिंतनशीलता ऋषिकाओं के स्वरूप को भी उपन्यास में स्थान दिया गया है। उस समय की संस्कृति में नारी को किस रूप में देखा जाता था और समाज में उसे कैसा स्थान प्राप्त था, को भी उपन्यास में दिखाया गया है।
उपर्युक्त विवरण की अभिव्यक्ति के साथ भाषा की व्यंजना शक्ति के साथ यदि भारत को वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक जीवन भी ध्वनित होता हो और पाठक इस रूप में लेना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।
इस उपन्यास को स्वरूप धारण करने में मेरी सहयोगिनी प्राध्यापिका श्रीमती डॉ. शशि इन्दुलिया, मेरी सुयोग्या शिष्या जयश्री कसेरा का जो सहयोग मिला वह स्तुत्य है। उपन्यास के मुद्रण और प्रकाशन में मेरे परम मित्र श्री महेन्द्र शर्मा, सेनानिवृत्त पुस्तकाध्यक्ष का सहयोग तो परम श्लघनीय है। अनेक बार तो इनके साथ मेरा जन्म, जन्मांतरों का संबंध प्रतीत होने लगता है। मैं इनके प्रति अपनी कृतज्ञता करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता।
इसी विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने भारतीय संस्कृति के अध्ययन और मनन का निश्चय किया। पाश्चात्य जर्मन विद्वान का कथन किसी सीमा तक सत्य प्रतीत होता है। कोई भी मानव-समुदाय अपने प्रारम्भिक काल में इतने उच्च विचार और सूक्ष्म अभिव्यक्ति में सक्षम नहीं हो सकता। इस विचार को ही आधार मानकर मैंने देव-संस्कृति और असुर-संस्कृति को काल्पनिक या अति आध्यात्मिक न मानकर विशुद्ध सांसारिक परिप्रेक्ष्य में देखा है। इन संस्कृतियों में मैंने उन त्रुटियों को दृष्टिगत किया जो किसी समुदाय की प्रारंभिक त्रुटियाँ होती हैं। मस्तीभरा जीवन, उपभोग्या नारी का स्वरूप, सोमरस का देवों द्वारा और सुरा का असुरों द्वारा पान, अनेक स्त्रियों के साथ अवैध संबंध आदि।
मैं यह मानकर चलता हूँ कि इन्हीं संस्कृतियों की त्रुटियों का निराकरण करते हुए महान् चिंतक एवं सिद्धांतनिष्ठ व्यक्तित्व के धनी परमश्रद्धेय वैवस्वत मनु के मन मानव-संस्कृति की स्थापना का श्रीगणेश किया। यदि मैं कहूँ कि मानव-संस्कृति देव-संस्कृति की त्रुटियों का ही संशोधित संस्करण है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रसिद्ध शायर इकबाल ने ठीक ही कहा है कि विश्व की बड़ी संस्कृतियाँ जहाँ से मिट गयीं, किन्तु इस संस्कृति में कुछ है कि आज भी जीवित है। इसी विचारधारा की अमिट छाप मेरे हृदयस्थल पर पड़ी है और मुझमें इस संस्कृति को जाँचने और परखने की बलवती इच्छा ने जनम लिया। इसी इच्छा का परिणाम ही इन दो पुस्तकों-महा अभियान एवं संघर्ष-का प्रणयन है। इस संस्कृति में बहुत उतार-चढ़ाव और संकट आये किन्तु यह अटूट और अजस्र गति से आज तक प्रवाहमान है।
मैं शरीर-विज्ञान का छात्र तो नहीं रहा किन्तु इस क्षेत्र में सोचने और विचारने का अधिकार तो मुझे प्रकृतिदत्त है। मैं अब यह और अधिक शक्ति के साथ मानने के लिये बाध्य हूँ कि हमारे रक्त में अपनों से, केवल अपनों से विद्रोह करने की क्षमता पुराकाल से ही चली आ रही है। इसका कारण तो मैं नहीं जानता किन्तु इतना अवश्य है कि इस संस्कृति में आदिकाल से ही इसके प्रति विद्रोह का भाव अनवरत गति से चला आ रहा है। महर्षि अत्रि ने वैवस्वत मनु के साथ इस मानव-संस्कृति की स्थापना की और उनके शिष्य ऋषि उतथ्य ने इसकी जड़ों को शक्तिशाली और बलवती बनाने का अदम्य प्रयास किया तब भी इसके विरोध के लिये विरोध हुआ। पुलस्त्य और विश्रवा ने अपनी पूर्ण शक्ति से मानव-संस्कृति का विरोध किया और रक्ष-संस्कृति की स्थापना की। इसका हमारा पुराण साहित्य साक्षी है। यही रक्ष-संस्कृति आगे चलकर आर्यों के लिये अत्यन्त बाधक सिद्ध हुई।
इस उपन्यास में मैंने इसी समय की मानव-संस्कृति को समुपस्थित करने का प्रयास किया है। इस समय के प्रमुख स्तम्भ थे, दक्षिण के यादव नरेश हैहयवंशी सह्स्रार्जुन, उत्तर के कान्यकुब्ज नरेश भरतवंशी गाधि और बाद में उनके पुत्र विश्वरथ, मध्यप्रदेश अयोध्या के नरेश अज, कौशल के नरेश तथा मिथिला नरेश निमि अथवा जनक। इन प्रमुख नरेशों के अतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे संघ-राज्यों का उदय भी आर्यावर्त की भूमि पर हो चुका था। उधर दूसरी ओर उच्च विचारधारा के उद्बोधक चिंतनशील मनीषियों ने भी इस पुण्य भूमि पर अवतरण किया, ये थे-अत्रि, वसिष्ठ, गृत्समद, अगस्त्य, विश्वामित्र, जाबाली, कपिल, याज्ञवल्कय, ऐतरेय, कणाद् आदि। स्त्री ऋषिकाओं में मदालसा, अपाला, लोपामुद्रा, अनसूया आदि।
साथ ही रक्ष-संस्कृति के अपूर्व योद्धा रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, विभीषण, मूल्यावन् आदि ने रक्ष-संस्कृति के प्रसार एवं प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और अभूतपूर्व वैज्ञानिक उन्नति का परिचय दिया। यक्षों में कुबेर को नहीं भुलाया जा सकता है। इतना सब होने पर भी सजग ऋषियों ने आर्य समाज में अंदर पनप रहे पारस्परिक वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष को आर्यों के सजग मनीषियों ने तुरंत चिह्नित कर लिया। राजाओं में पनप रहे सम्प्रभुता की भावना और एकांत भक्ति का धुव्रीकरण करने की कुत्सित भावना और फलस्वरूप ब्राह्मण में उत्पन्न पीड़ा हीनभावना को पहचाना और चिंतित हो उठे। ब्राह्मण युवकों में समुद्भूत विद्रोह के भाव, क्षत्रिय राजकुमारों के लिए और क्षत्रिय कुमारों में एवं राजाओं में ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या भाव तीव्रगति से उमड़ने लगा था चिंतनशील मनीषी ऋषियों को आर्यावर्त की संस्कृति के पैर डगमगाते दृष्टिगत होने लगे तथा सुसंगठित आर्य-संस्कृति के विघटन के चिह्न भी दिखाई देने लगे और इन दुष्प्रवृत्तियों के निराकरण के उपाय उपनिषदों और आरण्यकों के माध्यम से किये जाने के प्रयास प्रारंभ हो गये।
पुरा उत्तर कालीन संस्कृति के इसी रूप को प्रस्तुत उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया गया है। भारतीय समाज को सुदृढ़ता प्रदान करने के गौरवमय प्रयास को ऋषियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही भारतीय समाज में नारी की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। सुशिक्षिता तथा चिंतनशीलता ऋषिकाओं के स्वरूप को भी उपन्यास में स्थान दिया गया है। उस समय की संस्कृति में नारी को किस रूप में देखा जाता था और समाज में उसे कैसा स्थान प्राप्त था, को भी उपन्यास में दिखाया गया है।
उपर्युक्त विवरण की अभिव्यक्ति के साथ भाषा की व्यंजना शक्ति के साथ यदि भारत को वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक जीवन भी ध्वनित होता हो और पाठक इस रूप में लेना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।
इस उपन्यास को स्वरूप धारण करने में मेरी सहयोगिनी प्राध्यापिका श्रीमती डॉ. शशि इन्दुलिया, मेरी सुयोग्या शिष्या जयश्री कसेरा का जो सहयोग मिला वह स्तुत्य है। उपन्यास के मुद्रण और प्रकाशन में मेरे परम मित्र श्री महेन्द्र शर्मा, सेनानिवृत्त पुस्तकाध्यक्ष का सहयोग तो परम श्लघनीय है। अनेक बार तो इनके साथ मेरा जन्म, जन्मांतरों का संबंध प्रतीत होने लगता है। मैं इनके प्रति अपनी कृतज्ञता करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता।
जगदीशप्रसाद कौशिक
संघर्ष
ऋषिराज अब अधिक सोचने का अवसर नहीं है। यदि आपने मेरे प्रस्ताव को गंभीरता
से नहीं लिया तो आर्य-संस्कृति छिन्न-भिन्न हो जाएगी। हमारे आश्रमों में
अस्त्र-शस्त्रों का विपुल भंडार है। जनता का पूर्ण सहयोग हमारे साथ है।
केवल कमी है तो सैन्य-संगठन की है। यदि आप आज्ञा करें तो इसका गठन भी कोई
अनहोनी घटना या कठिन कार्य नहीं है। सभी आश्रमों को निर्देश दिये जा सकते
है कि वे अपनी आश्रम-सेनाएँ गठित करें। अस्त्र-संचालन का प्रशिक्षण केवल
क्षत्रिय राजकुमारों को ही क्यों ? अच्छा तो यह हो कि क्षत्रिय कुमारों के
धनुर्वेद प्रशिक्षण को प्रतिबंधित कर दिया जाए और धनुर्विद्या का
प्रशिक्षण ऋषि कुमारों एवं अन्य वर्णों के नवयुवकों को भी दिया जाना
प्रारम्भ कर दिया जाए। ऐसा करने पर ही हम उमड़ते हुए क्षत्रिय-विद्रोह को
निराकृत करने में सफल हो सकेंगे। महर्षि कणाद् इतना कुछ एक साँस में ही कह
गए। उस समय ऐसा अनुभव हो रहा था कि ऋषि अत्यन्त उत्तेजित हैं और किसी भावी
संकट के आगमन को चित्रवत् अपनी आँखों के सामने देखते हुए उससे संत्रास की
प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहे हैं।
महर्षि कणाद् ने अपना वक्तव्य समाप्त कर महर्षि भरद्वाज की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा। पद्मासन लगाये कुशासन पर स्थित महर्षि भरद्वाज अत्यंत शान्ति के साथ महर्षि कणाद् के कथन को सुन रहे थे कणाद् के अंतर्मन की पीड़ा को भली प्रकार से समझ भी रहे थे किन्तु जनकल्याण की भावना से उत्पन्न प्रभामंडल से आवृत्त उनकी मुखाकृति और ललाट पर उभरी हुई चिंतन की रेखाएँ इस ओर इंगित कर रही थी कि महर्षि के अंतर्मन में कुछ और ही द्वंद्व अठखेलियाँ कर रहा था। महर्षि का मन कणाद् से भी अधिक आहत था, किन्तु वे अनुशासन की श्रृंखला में आबद्धकर स्वतंत्र विचरण का अवसर नहीं देना चाहते थे। महर्षि इस बात को भली-भाँति जानते थे कि कणाद् एक चिंतनशील मनीषी तो हैं किन्तु वे राजनीतिक बारीकियों को चिह्नित करने में पारगंत नहीं हैं। दूसरे, महर्षि कणाद् को इसलिए तो आहूत नहीं किया था कि वे यहाँ आकर उनसे राजनीति पर वार्तालाप करें। वे तो केवल परमाणु के संबंध में उनकी उपलब्धियों का लेखा-जोखा मात्र लेना चाहते थे। साथ ही वे यह भी सोच रहे थे कि क्या कणाद् अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं ?
सिद्धांत निर्माताओं का सक्रिय राजनीति में प्रवेश कराना और सत्ता प्राप्ति की ओर उन्मुख होना देश के लिए शुभ नहीं होता। सिद्धांत निर्माताओं और आविष्कर्ताओं को जब सत्ता-सुख का अनुभव होने लगता है तथा देश, समाज, संस्कृति का ह्नास प्रारंभ हो जाता है। सत्ता-सुख तो केवल अबुद्धजनों की विरासत होती है। सत्ता तो एक धरोहर होती है जो केवल उन लोगों को ही सौंपी जा सकती है जिनका चिंतन के साथ दूर का संबंध नहीं होता। फलत: चिंतनशील मनीषियों का उन पर मात्र अंकुश होता है।
वे सत्ता के अंशधारी नहीं होते जिस प्रकार महावत। सत्ता की बागडोर सहिष्णु, त्यागी, देशभक्त, सामजसेवी ब्राह्मणों के हाथ में रहती है जो मात्र उसका सत्ता का संचालन भर करते है किन्तु सत्ता-सुख की भागीदार नहीं होते। तपस्या उनका धर्म होता है और सेवा उनका कर्म। ‘सर्वे भवन्तु सुखिनो’ ही उनका मूल-मंत्र होता है। तभी संस्कृति एकता के सूत्र में बँधकर प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करती है। ऐसी अनेक धारणाएँ महर्षि को मन में हिचकोले ले रही थी। ठीक इसी समय कणाद् का वक्तव्य समाप्त हुआ था। महर्षि ने कणाद् की ओर दर्द भरी दृष्टि से देखा। कणाद् क्षणभर के लिए अस्त-व्यस्त हो गये जैसे महर्षि की दृष्टि ने कणाद् को एक अपराधी के रूप में चिह्नित किया हो, किन्तु कणाद् ने शीघ्र ही अपने को आश्वस्त कर लिया और इस प्रकार का आभास देने का प्रयास किया कि जैसे उनमें घबराहट ने प्रवेश ही नहीं किया हो। कणाद् ने देखा महर्षि के ओठों पर कुछ कहने की इच्छा से कंपन तैरने लगा है और तत्क्षण ही कणाद् के श्रुति कुहर में शांत गंभीर वाणी ने प्रवेश किया।
महर्षि कणाद् ने अपना वक्तव्य समाप्त कर महर्षि भरद्वाज की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा। पद्मासन लगाये कुशासन पर स्थित महर्षि भरद्वाज अत्यंत शान्ति के साथ महर्षि कणाद् के कथन को सुन रहे थे कणाद् के अंतर्मन की पीड़ा को भली प्रकार से समझ भी रहे थे किन्तु जनकल्याण की भावना से उत्पन्न प्रभामंडल से आवृत्त उनकी मुखाकृति और ललाट पर उभरी हुई चिंतन की रेखाएँ इस ओर इंगित कर रही थी कि महर्षि के अंतर्मन में कुछ और ही द्वंद्व अठखेलियाँ कर रहा था। महर्षि का मन कणाद् से भी अधिक आहत था, किन्तु वे अनुशासन की श्रृंखला में आबद्धकर स्वतंत्र विचरण का अवसर नहीं देना चाहते थे। महर्षि इस बात को भली-भाँति जानते थे कि कणाद् एक चिंतनशील मनीषी तो हैं किन्तु वे राजनीतिक बारीकियों को चिह्नित करने में पारगंत नहीं हैं। दूसरे, महर्षि कणाद् को इसलिए तो आहूत नहीं किया था कि वे यहाँ आकर उनसे राजनीति पर वार्तालाप करें। वे तो केवल परमाणु के संबंध में उनकी उपलब्धियों का लेखा-जोखा मात्र लेना चाहते थे। साथ ही वे यह भी सोच रहे थे कि क्या कणाद् अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं ?
सिद्धांत निर्माताओं का सक्रिय राजनीति में प्रवेश कराना और सत्ता प्राप्ति की ओर उन्मुख होना देश के लिए शुभ नहीं होता। सिद्धांत निर्माताओं और आविष्कर्ताओं को जब सत्ता-सुख का अनुभव होने लगता है तथा देश, समाज, संस्कृति का ह्नास प्रारंभ हो जाता है। सत्ता-सुख तो केवल अबुद्धजनों की विरासत होती है। सत्ता तो एक धरोहर होती है जो केवल उन लोगों को ही सौंपी जा सकती है जिनका चिंतन के साथ दूर का संबंध नहीं होता। फलत: चिंतनशील मनीषियों का उन पर मात्र अंकुश होता है।
वे सत्ता के अंशधारी नहीं होते जिस प्रकार महावत। सत्ता की बागडोर सहिष्णु, त्यागी, देशभक्त, सामजसेवी ब्राह्मणों के हाथ में रहती है जो मात्र उसका सत्ता का संचालन भर करते है किन्तु सत्ता-सुख की भागीदार नहीं होते। तपस्या उनका धर्म होता है और सेवा उनका कर्म। ‘सर्वे भवन्तु सुखिनो’ ही उनका मूल-मंत्र होता है। तभी संस्कृति एकता के सूत्र में बँधकर प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करती है। ऐसी अनेक धारणाएँ महर्षि को मन में हिचकोले ले रही थी। ठीक इसी समय कणाद् का वक्तव्य समाप्त हुआ था। महर्षि ने कणाद् की ओर दर्द भरी दृष्टि से देखा। कणाद् क्षणभर के लिए अस्त-व्यस्त हो गये जैसे महर्षि की दृष्टि ने कणाद् को एक अपराधी के रूप में चिह्नित किया हो, किन्तु कणाद् ने शीघ्र ही अपने को आश्वस्त कर लिया और इस प्रकार का आभास देने का प्रयास किया कि जैसे उनमें घबराहट ने प्रवेश ही नहीं किया हो। कणाद् ने देखा महर्षि के ओठों पर कुछ कहने की इच्छा से कंपन तैरने लगा है और तत्क्षण ही कणाद् के श्रुति कुहर में शांत गंभीर वाणी ने प्रवेश किया।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book