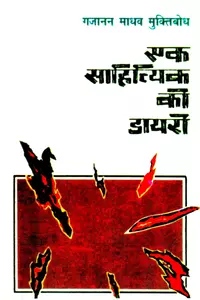|
कहानी संग्रह >> काठ का सपना काठ का सपनागजानन माधव मुक्तिबोध
|
148 पाठक हैं |
||||||
मुक्तिबोध के जीवन के अन्तिम समय तक उनके द्वारा लिखी गयी कुछ-एक श्रेष्ठ कहानियों का संग्रह है - ‘काठ का सपना’।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मुक्तिबोध के जीवन के अन्तिम समय तक उनके द्वारा लिखी गई कुछेक श्रेष्ठ
कहानियों का संग्रह है "काठ का सपना।" अभिव्यक्ति के माध्यम के नाते जहाँ
कविता हारी वहाँ मुक्तिबोध ने डायरी विधा पकड़ी और जब यह भी पूरी न पड़ी
तब कहानी को अपनाया।
सच तो यह है कि युग के ढँके-उघड़े वास्तविक स्वरूप का, स्वयं झेल-झेल कर, जितनी समग्रता के साथ उन्होंने अनुभव किया और उसे अभिव्यक्ति देने की जितनी बेचैनी उनमें थी उसके आगे साहित्य की परिचित विधा-सीमाएँ टूट गयीं। मुक्तिबोध की कविता बढ़कर डायरी बन चलती है, डायरी में कहानी झाँक उठेगी, और कहानी मानो किसी विषय विशेष का चिन्तन जो गहराई और विस्तार में उत्तरोत्तर बढ़तर जाए। मुक्तिबोध का सारा साहित्य वस्तुतः एक अभिशप्त जीवन जीनेवाले अत्यन्त संवेदनशील सामाजिक व्यक्ति का चिन्तन विवेचन है; और यह भी कहीं निराले में या किसी अन्य के साथ बैठकर नहीं, अपने पीड़ा संघर्षों भरे परिवेश में रहते और अपने से ऊपर उठकर स्वयं अपने से जूझते हुए किया गया है। उनकी ये कहानियाँ इसी बात को रेखांकित करती हैं।
प्रस्तुत है भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’ और ‘एक साहित्यिक की डायरी’ के बाद यह संग्रह ‘‘काठ का सपना’ मुक्तिबोध द्वारा लिखित मनुष्यता का दस्तावेज का एक और पृष्ठ !
मुक्तिबोध की कहानियों का रचनाकार बीस वर्षों में फैला हुआ है। इसीलिए कहानियों के स्तर में फर्क है। इसी संग्रह की कुछ कहानियाँ 1943-’44 की है, जबकि कुछ उन्होंने अपनी बीमारी के पहले 1962’63 में समाप्त की थीं। जमाने के साथ कहानी का कौशल भी बदल गया। इस बदले हुए कौशल की कहानियाँ हैं, ‘‘काठ का सपना’’ और ‘‘पक्षी और दीमक’’।
मुक्तिबोध की हर रचना साहित्य की सभी विधाओं को एक अजीब चुनौती है।
मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है; कविता बढ़ते-बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते-चलते कहानी हो जाती है। डायरी कहानी और उपन्यास तीनों के गुण-दोषों से बेलाग ‘विपात्र’ की कल्पना मुक्तिबोध ने उपन्यास के रूप में की थी। वह उसे छपाना भी चाहते थे उपन्यास कहकर। लम्बे-लम्बे पृष्ठों पर बड़े बड़े हर्फों में लिखी हुई यह कहानी अपनी विशालकाय पाण्डुलिपि में उपन्यास ही लगती थी। मगर टाइप कराने पर मालूम हुआ कि उसे अधिक से अधिक एक लम्बी कहानी के बतौर ही छापा जा सकता है।
सचाई यह है कि ‘विपात्र’ कहानी या उपन्यास दोनों में से कुछ भी न होने के बावजूद दोनों ही है। कहानी और उपन्यास दोनों की संकीर्ण परिभाषाएँ किस तरह टूट रही हैं और साहित्य की विधाएँ कैसे एक-दूसरे के नजदीक आती हुई गुमनाम होती जा रही हैं, इसे मुक्तिबोध जैसे द्रष्टा कलाकार ही पहचान सकते थे।
1959 से 1962 के बीच ‘विपात्र’ को मुक्तिबोध ने तीन बार लिखा था। मैंने इस संग्रह में उसका तीसरा और आखिरी प्रारूप शामिल किया है। इस प्रारूप में भी मुक्तिबोध कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। मगर उनकी बीमारी के कारण यह सम्भव न हो सका।
‘ब्रह्मराक्षस’ मुक्तिबोध का प्रिय पात्र है; कविता, कहानी हर कहीं ब्रह्मराक्षस का जिक्र है ! ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’ में ‘ब्रह्मराक्षस’ को सम्बोधित एक कविता है और इस संग्रह में ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ को लेकर एक कहानी है। मुक्तिबोध ने जिस तरह का अभिशप्त और निर्वासित जीवन जिया उसे, उसकी पीड़ा को, एक ब्रह्मराक्षस ही समझ सकता है।
सच तो यह है कि युग के ढँके-उघड़े वास्तविक स्वरूप का, स्वयं झेल-झेल कर, जितनी समग्रता के साथ उन्होंने अनुभव किया और उसे अभिव्यक्ति देने की जितनी बेचैनी उनमें थी उसके आगे साहित्य की परिचित विधा-सीमाएँ टूट गयीं। मुक्तिबोध की कविता बढ़कर डायरी बन चलती है, डायरी में कहानी झाँक उठेगी, और कहानी मानो किसी विषय विशेष का चिन्तन जो गहराई और विस्तार में उत्तरोत्तर बढ़तर जाए। मुक्तिबोध का सारा साहित्य वस्तुतः एक अभिशप्त जीवन जीनेवाले अत्यन्त संवेदनशील सामाजिक व्यक्ति का चिन्तन विवेचन है; और यह भी कहीं निराले में या किसी अन्य के साथ बैठकर नहीं, अपने पीड़ा संघर्षों भरे परिवेश में रहते और अपने से ऊपर उठकर स्वयं अपने से जूझते हुए किया गया है। उनकी ये कहानियाँ इसी बात को रेखांकित करती हैं।
प्रस्तुत है भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’ और ‘एक साहित्यिक की डायरी’ के बाद यह संग्रह ‘‘काठ का सपना’ मुक्तिबोध द्वारा लिखित मनुष्यता का दस्तावेज का एक और पृष्ठ !
मुक्तिबोध की कहानियों का रचनाकार बीस वर्षों में फैला हुआ है। इसीलिए कहानियों के स्तर में फर्क है। इसी संग्रह की कुछ कहानियाँ 1943-’44 की है, जबकि कुछ उन्होंने अपनी बीमारी के पहले 1962’63 में समाप्त की थीं। जमाने के साथ कहानी का कौशल भी बदल गया। इस बदले हुए कौशल की कहानियाँ हैं, ‘‘काठ का सपना’’ और ‘‘पक्षी और दीमक’’।
मुक्तिबोध की हर रचना साहित्य की सभी विधाओं को एक अजीब चुनौती है।
मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है; कविता बढ़ते-बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते-चलते कहानी हो जाती है। डायरी कहानी और उपन्यास तीनों के गुण-दोषों से बेलाग ‘विपात्र’ की कल्पना मुक्तिबोध ने उपन्यास के रूप में की थी। वह उसे छपाना भी चाहते थे उपन्यास कहकर। लम्बे-लम्बे पृष्ठों पर बड़े बड़े हर्फों में लिखी हुई यह कहानी अपनी विशालकाय पाण्डुलिपि में उपन्यास ही लगती थी। मगर टाइप कराने पर मालूम हुआ कि उसे अधिक से अधिक एक लम्बी कहानी के बतौर ही छापा जा सकता है।
सचाई यह है कि ‘विपात्र’ कहानी या उपन्यास दोनों में से कुछ भी न होने के बावजूद दोनों ही है। कहानी और उपन्यास दोनों की संकीर्ण परिभाषाएँ किस तरह टूट रही हैं और साहित्य की विधाएँ कैसे एक-दूसरे के नजदीक आती हुई गुमनाम होती जा रही हैं, इसे मुक्तिबोध जैसे द्रष्टा कलाकार ही पहचान सकते थे।
1959 से 1962 के बीच ‘विपात्र’ को मुक्तिबोध ने तीन बार लिखा था। मैंने इस संग्रह में उसका तीसरा और आखिरी प्रारूप शामिल किया है। इस प्रारूप में भी मुक्तिबोध कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। मगर उनकी बीमारी के कारण यह सम्भव न हो सका।
‘ब्रह्मराक्षस’ मुक्तिबोध का प्रिय पात्र है; कविता, कहानी हर कहीं ब्रह्मराक्षस का जिक्र है ! ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’ में ‘ब्रह्मराक्षस’ को सम्बोधित एक कविता है और इस संग्रह में ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ को लेकर एक कहानी है। मुक्तिबोध ने जिस तरह का अभिशप्त और निर्वासित जीवन जिया उसे, उसकी पीड़ा को, एक ब्रह्मराक्षस ही समझ सकता है।
बावड़ी में वह स्वयं
पागल प्रतीकों में निरन्तर कह रहा
वह कोठरी में किस तरह
अपना गणित करता रहा
और मर गया....
वह सघन झाड़ी के कँटीले
तम-विवर में
मरे पक्षी-सा
बिदा ही हो गया
वह ज्योति अनजानी सदा को सो गयी
यह क्यों हुआ !
क्यों यह हुआ !!
मैं ब्रह्माराक्षस का सजल उर शिष्य
होना चाहता
जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य,
उसकी वेदना का स्रोत
संगत, पूर्ण निष्कर्षों तलक
पहुँचा सकूँ।
(ब्रह्मराक्षस’: ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’, पृष्ठ 17)
पागल प्रतीकों में निरन्तर कह रहा
वह कोठरी में किस तरह
अपना गणित करता रहा
और मर गया....
वह सघन झाड़ी के कँटीले
तम-विवर में
मरे पक्षी-सा
बिदा ही हो गया
वह ज्योति अनजानी सदा को सो गयी
यह क्यों हुआ !
क्यों यह हुआ !!
मैं ब्रह्माराक्षस का सजल उर शिष्य
होना चाहता
जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य,
उसकी वेदना का स्रोत
संगत, पूर्ण निष्कर्षों तलक
पहुँचा सकूँ।
(ब्रह्मराक्षस’: ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’, पृष्ठ 17)
अभिशप्त मनुष्य की ‘वेदना का स्रोत’ और संगत पूर्ण
निष्कर्षों
की खोज की विवशता के कारण ही मुक्तिबोध के सारे साहित्य में एक ही विशाल
अनुभव की सैकड़ों सूरतें हैं। शायद ही किसी कलाकार ने अपने अनुभव को आखिरी
निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए इस हद तक निचोड़ा है, जिस हद तक मुक्तिबोध ने
निचोड़ा है-यहाँ तक कि इस प्रयत्न में स्वयं मुक्तिबोध पूरी तरह निचुड़
गये।
सचाई यह है कि मुक्तिबोध स्वयं ही ब्रह्मराक्षस थे और स्वयं ही ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ भी। कविता में जो काम अधूरा रह गया उसे उन्होंने डायरी में पूरा करने का प्रयत्न किया और डायरी में जो रह गया उसे शकल देने के लिए उन्होंने कहानी का माध्यम चुना-हालाँकि ये तीनों ही विधाएँ मुक्तिबोध के उस महानुभव की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जगह-जगह अपर्याप्त साबित हुई हैं जिसे किसी युग का समग्र अनुभव कहा जा सकता है। मुक्तिबोध अकेले कलाकार हैं
जिनके अनुभव का आवेग अभिव्यक्ति की क्षमता से इतना बड़ा था कि सारा साहित्य टूट गया। मुक्तिबोध के साहित्य को कसौटी के रूप में स्वीकार करना खतरे से खाली नहीं। उसमें इतनी प्रचण्डता है कि उस पर परखने पर अपने अन्य गुणों के लिए महत्त्वपूर्ण दूसरों के साहित्य निश्चित ही टुच्चा नजर आएगा। बुद्धिमानी इसी में है कि मुक्तिबोध के साहित्य को उनके ही साहित्य की कसौटी के रूप में देखा जाए।
मुक्तिबोध अभिव्यक्ति की जिस बेचैनी से पीड़ित थे, ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ उसी की कहानी है। चेखॅव की ‘घोड़ा’ यदि साधारण आदमी के दर्द की अभिव्यक्ति की सबसे उम्दा कहानी है तो ‘ब्रह्माराक्षस का शिष्य’ कलाकार की अभिव्यक्ति की बेचैनी की सबसे अर्थगर्भित कहानी है। उस कलाकार से अधिक अकेला कौन हो सकता है जो यह अनुभव करता हो कि वह अपने अनुभव के आगे गूँगा है। उसका सारा जीवन एक भुतहा मकान है और वह खुद महज एक ब्रह्मराक्षस है ! मुक्तिबोध की कहानी का ‘ब्रह्माराक्षस’ भी दरअसल एक कलाकार है जिसे केवल अभिव्यक्ति ही मुक्त कर सकती है। उसका शिष्य उसकी अभिव्यक्ति है :
"गुरु ने दुःखपूर्ण कोमलता से कहा, "शिष्य ! स्पष्ट कर दूँ कि मैं ब्रह्माराक्षस हूँ; किन्तु फिर भी तुम्हारा गुरु हूँ। मुझे तुम्हारा स्नेह चाहिए। अपने मानव जीवन में मैंने विश्व की समस्त विद्या को मथ डाला; किन्तु दुर्भाग्य से कोई योग्य शिष्य न मिल पाया कि जिसे मैं समस्त ज्ञान दे पाता। इसीलिए मेरी आत्मा इस संसार में अटकी रह गयी और मैं ब्रह्मराक्षस के रूप में यहाँ विराजमान रहा।"
अभिव्यक्ति मुक्तिबोध की निगाह में मुक्ति थी; मगर उसकी सार्थकता दूसरों के सन्दर्भ में थी। अपने आप में वह भी एक दूसरे किस्म का अभिशाप थी। इसीलिए शिष्य को ‘ज्ञान-दान’ देता हुआ कहानी का ‘ब्रह्मराक्षस’ कहता है :
"मैंने अज्ञान से तुम्हारी मुक्ति की। तुमने मेरा ज्ञान प्राप्त कर मेरी आत्मा को मुक्ति दिला दी। ज्ञान का लाया हुआ उत्तरदायित्व मैंने पूरा किया। अब मेरा यह उत्तरदायित्व तुम पर आ गया है। जब तक मेरा दिया हुआ तुम किसी और को न दोगे, तुम्हारी मुक्ति नहीं।"
मुक्तिबोध का विश्वास भी था कि कोई भी अभिव्यक्ति अपने व्यापक सन्दर्भों में ही सार्थक है; अपने तमाम सन्दर्भों से कटी हुई मनोदशा केवल एक धुन्ध है। ‘एक साहित्यिक की डायरी’ में ‘नयी कहानी’ पर बहस करते हुए उन्होंने लिखा है :
"नयी कहानी में अधुनिक मानव (इसका मतलब चाहे जो लीजिए, प्रगतिवादी अर्थ मत लीजिए) की जो विचित्र मनोदशा है उसको अगर आप उसके सारे सन्दर्भों से काटकर, उसके सारे ब्रह्मा सामाजिक-पारिवारिक इत्यादि सम्बन्धों से काटकर, उस मनोदशा को मानो अधर में लटकाकर विचित्र करेंगे तो मनोदशा के नाम पर (कहानी में) एक धुन्ध समा जाएगा। कहानी में अगर सिर्फ भीतरी धुन्ध हो और सिर्फ वही वह रहे और उसी की इतनी प्रधानता हो कि वस्तु-सत्यों के
संवेदनात्मक चित्रों का प्रायः लोप हो जाए तो आप वही गलती करेंगे कि जो (मेरे खयाल से) नयी कविता ने की। कविता की कला कथा की कला से अधिक अमूर्त तो वैसे ही होती है, इसलिए सम्भवतः वे बातें खप भी जाती हैं। किन्तु कहानी में ?"
(विशिष्ट और अद्वितीय : पृष्ठ 108)
अजीब संयोग है कि इस संग्रह की सबसे अच्छी कहानी ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ सबसे पहले बच्चों की एक पत्रिका में छपी थी। कारण जो भी हो और कहानी छपी जहां भी हो, लिखी वह गयी थी अपने-आप से बहस के लिए। एक तरह से मुक्तिबोध की सारी कविताएँ और अन्य रचनाएँ अपने-आप से जिरह हैं। जैसे ज्याँ पॉल सार्त्र का सारा साहित्य एक लम्बी जिरह है उसी तरह मुक्तिबोध का साहित्य एक अन्तहीन बहस है। फर्क इतना है कि सार्त्र की अनुगूँजें बौद्धिक हैं, मुक्तिबोध की शंकाएँ एक कवि की हैं।
कुछ चीजों से मुक्तिबोध को एलर्जी थी जिनमें सबसे पहला नम्बर है सफलता का। सामाजिक सफलता से मुक्तिबोध को जो दहशत थी उसकी छाप हर जगह है। समृद्ध होकर जीने के लिए आदमी को जो कीमत चूकानी पड़ती है वह हमेशा ही मुक्तिबोध की परेशानी का विषय रही। ‘पक्षी और दीमक’ के जरिए इस परेशानी और दहशत को समझा जा सकता है। और इसी से यह भी समझा जा सकता है कि सामाजिक सफलता के रास्ते में भागकर मुक्तिबोध ने क्यों निर्वासित होना पसन्द किया। अपनी एक कम विख्यात कविता में भी मुक्तिबोध ने अपने इस भय को व्यक्त किया है :
सचाई यह है कि मुक्तिबोध स्वयं ही ब्रह्मराक्षस थे और स्वयं ही ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ भी। कविता में जो काम अधूरा रह गया उसे उन्होंने डायरी में पूरा करने का प्रयत्न किया और डायरी में जो रह गया उसे शकल देने के लिए उन्होंने कहानी का माध्यम चुना-हालाँकि ये तीनों ही विधाएँ मुक्तिबोध के उस महानुभव की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जगह-जगह अपर्याप्त साबित हुई हैं जिसे किसी युग का समग्र अनुभव कहा जा सकता है। मुक्तिबोध अकेले कलाकार हैं
जिनके अनुभव का आवेग अभिव्यक्ति की क्षमता से इतना बड़ा था कि सारा साहित्य टूट गया। मुक्तिबोध के साहित्य को कसौटी के रूप में स्वीकार करना खतरे से खाली नहीं। उसमें इतनी प्रचण्डता है कि उस पर परखने पर अपने अन्य गुणों के लिए महत्त्वपूर्ण दूसरों के साहित्य निश्चित ही टुच्चा नजर आएगा। बुद्धिमानी इसी में है कि मुक्तिबोध के साहित्य को उनके ही साहित्य की कसौटी के रूप में देखा जाए।
मुक्तिबोध अभिव्यक्ति की जिस बेचैनी से पीड़ित थे, ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ उसी की कहानी है। चेखॅव की ‘घोड़ा’ यदि साधारण आदमी के दर्द की अभिव्यक्ति की सबसे उम्दा कहानी है तो ‘ब्रह्माराक्षस का शिष्य’ कलाकार की अभिव्यक्ति की बेचैनी की सबसे अर्थगर्भित कहानी है। उस कलाकार से अधिक अकेला कौन हो सकता है जो यह अनुभव करता हो कि वह अपने अनुभव के आगे गूँगा है। उसका सारा जीवन एक भुतहा मकान है और वह खुद महज एक ब्रह्मराक्षस है ! मुक्तिबोध की कहानी का ‘ब्रह्माराक्षस’ भी दरअसल एक कलाकार है जिसे केवल अभिव्यक्ति ही मुक्त कर सकती है। उसका शिष्य उसकी अभिव्यक्ति है :
"गुरु ने दुःखपूर्ण कोमलता से कहा, "शिष्य ! स्पष्ट कर दूँ कि मैं ब्रह्माराक्षस हूँ; किन्तु फिर भी तुम्हारा गुरु हूँ। मुझे तुम्हारा स्नेह चाहिए। अपने मानव जीवन में मैंने विश्व की समस्त विद्या को मथ डाला; किन्तु दुर्भाग्य से कोई योग्य शिष्य न मिल पाया कि जिसे मैं समस्त ज्ञान दे पाता। इसीलिए मेरी आत्मा इस संसार में अटकी रह गयी और मैं ब्रह्मराक्षस के रूप में यहाँ विराजमान रहा।"
अभिव्यक्ति मुक्तिबोध की निगाह में मुक्ति थी; मगर उसकी सार्थकता दूसरों के सन्दर्भ में थी। अपने आप में वह भी एक दूसरे किस्म का अभिशाप थी। इसीलिए शिष्य को ‘ज्ञान-दान’ देता हुआ कहानी का ‘ब्रह्मराक्षस’ कहता है :
"मैंने अज्ञान से तुम्हारी मुक्ति की। तुमने मेरा ज्ञान प्राप्त कर मेरी आत्मा को मुक्ति दिला दी। ज्ञान का लाया हुआ उत्तरदायित्व मैंने पूरा किया। अब मेरा यह उत्तरदायित्व तुम पर आ गया है। जब तक मेरा दिया हुआ तुम किसी और को न दोगे, तुम्हारी मुक्ति नहीं।"
मुक्तिबोध का विश्वास भी था कि कोई भी अभिव्यक्ति अपने व्यापक सन्दर्भों में ही सार्थक है; अपने तमाम सन्दर्भों से कटी हुई मनोदशा केवल एक धुन्ध है। ‘एक साहित्यिक की डायरी’ में ‘नयी कहानी’ पर बहस करते हुए उन्होंने लिखा है :
"नयी कहानी में अधुनिक मानव (इसका मतलब चाहे जो लीजिए, प्रगतिवादी अर्थ मत लीजिए) की जो विचित्र मनोदशा है उसको अगर आप उसके सारे सन्दर्भों से काटकर, उसके सारे ब्रह्मा सामाजिक-पारिवारिक इत्यादि सम्बन्धों से काटकर, उस मनोदशा को मानो अधर में लटकाकर विचित्र करेंगे तो मनोदशा के नाम पर (कहानी में) एक धुन्ध समा जाएगा। कहानी में अगर सिर्फ भीतरी धुन्ध हो और सिर्फ वही वह रहे और उसी की इतनी प्रधानता हो कि वस्तु-सत्यों के
संवेदनात्मक चित्रों का प्रायः लोप हो जाए तो आप वही गलती करेंगे कि जो (मेरे खयाल से) नयी कविता ने की। कविता की कला कथा की कला से अधिक अमूर्त तो वैसे ही होती है, इसलिए सम्भवतः वे बातें खप भी जाती हैं। किन्तु कहानी में ?"
(विशिष्ट और अद्वितीय : पृष्ठ 108)
अजीब संयोग है कि इस संग्रह की सबसे अच्छी कहानी ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ सबसे पहले बच्चों की एक पत्रिका में छपी थी। कारण जो भी हो और कहानी छपी जहां भी हो, लिखी वह गयी थी अपने-आप से बहस के लिए। एक तरह से मुक्तिबोध की सारी कविताएँ और अन्य रचनाएँ अपने-आप से जिरह हैं। जैसे ज्याँ पॉल सार्त्र का सारा साहित्य एक लम्बी जिरह है उसी तरह मुक्तिबोध का साहित्य एक अन्तहीन बहस है। फर्क इतना है कि सार्त्र की अनुगूँजें बौद्धिक हैं, मुक्तिबोध की शंकाएँ एक कवि की हैं।
कुछ चीजों से मुक्तिबोध को एलर्जी थी जिनमें सबसे पहला नम्बर है सफलता का। सामाजिक सफलता से मुक्तिबोध को जो दहशत थी उसकी छाप हर जगह है। समृद्ध होकर जीने के लिए आदमी को जो कीमत चूकानी पड़ती है वह हमेशा ही मुक्तिबोध की परेशानी का विषय रही। ‘पक्षी और दीमक’ के जरिए इस परेशानी और दहशत को समझा जा सकता है। और इसी से यह भी समझा जा सकता है कि सामाजिक सफलता के रास्ते में भागकर मुक्तिबोध ने क्यों निर्वासित होना पसन्द किया। अपनी एक कम विख्यात कविता में भी मुक्तिबोध ने अपने इस भय को व्यक्त किया है :
‘उन्नति’ के क्षेत्रों में
‘प्रतिष्ठा’ के क्षेत्रों में
मानव की छाती की बहती है न कहीं गन्ध
केवल मनुष्य-हीन निर्जन प्रसारों पर
आँख से एक ही
दुनिया को निहारती फैली है-
बुद्धि की कीर्ति की, सफलता की, समृद्धि की
पूनों की चाँदनी !
............................
मुझको डर लगता है
कहीं मैं भी तो सफलता के चन्द्र की छाया में
घुग्घू या सियार या भूत न कहीं बन जाऊँ।
(‘कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं’: ‘नयी दिशा’ संख्या 1, 1955)
‘प्रतिष्ठा’ के क्षेत्रों में
मानव की छाती की बहती है न कहीं गन्ध
केवल मनुष्य-हीन निर्जन प्रसारों पर
आँख से एक ही
दुनिया को निहारती फैली है-
बुद्धि की कीर्ति की, सफलता की, समृद्धि की
पूनों की चाँदनी !
............................
मुझको डर लगता है
कहीं मैं भी तो सफलता के चन्द्र की छाया में
घुग्घू या सियार या भूत न कहीं बन जाऊँ।
(‘कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं’: ‘नयी दिशा’ संख्या 1, 1955)
मुक्तिबोध की दो कहानियाँ, ‘विपात्र’ और
‘क्लॉड
ईथराली’ दो तरह के संकटों को पेश करती हैं : एक बुद्धिजीवी का
संकट
और दूसरा समूची मानव-सभ्यता का संकट जिसका प्रतिनिधि है क्लॉड ईथरली।
बुद्धिजीवी के संकट को, जिसे आचरण का संकट कहना ज्यादा सही होगा,
मुक्तिबोध ने और भी जगह अपनी रचना का विषय बनाया है। मगर
‘क्लॉ़ड
ईथरली’ के जरिये उन्होंने समूची सभ्यता को नंगा कर दिया है।
क्लॉड
ईथरली चाबुक की तरह है जो जख्म-जैसी स्मृति छोड़ जाता है।
मुक्तिबोध की कहानियों में जगह-जगह आवेश है, उतावलापन है, निस्संगता की कमी है-यहाँ तक कि कहानी की कमी है। और उनकी कहानियों का मूल्यांकन करते समय उनकी खामियों को नजर अन्दाज भी नहीं किया जा सकता। मगर क्या मुक्तिबोध के साहित्य का, जो महज साहित्य न रहकर मनुष्यता का दस्तावेज हो गया है, मूल्यांकन करने की जरूरत रह गयी है ?
मुक्तिबोध की कहानियों में जगह-जगह आवेश है, उतावलापन है, निस्संगता की कमी है-यहाँ तक कि कहानी की कमी है। और उनकी कहानियों का मूल्यांकन करते समय उनकी खामियों को नजर अन्दाज भी नहीं किया जा सकता। मगर क्या मुक्तिबोध के साहित्य का, जो महज साहित्य न रहकर मनुष्यता का दस्तावेज हो गया है, मूल्यांकन करने की जरूरत रह गयी है ?
नयी दिल्ली
30 नवम्बर, 1966
30 नवम्बर, 1966
-श्रीकान्त वर्मा
क्लॉड ईथरली
पीली धूप से चमकती हुई ऊँची भीत जिसके नीले फ्रेम में काँचवाले रोशनदान
दूर सड़क से दीखते हैं।
मैं सड़क पार कर लेता हूँ। जंगली, बेमहक लेकिन खूबसूरत विदेशी फूलों के नीचे ठहर-सा जाता हूँ कि जो फूल, भीत के पासवाले अहाते की आदमकद दीवार के ऊपर फैले सड़क के बाजू पर बाँहें बिछाकर झुक गये हैं। पता नहीं कैसे, किस साहस से व क्यों उसी अहाते के पास बिजली का ऊँचा खम्भा—जो पाँच-छह दिशाओं में जानेवाली सूनी सड़कों पर तारों की सीधी लकीरें भेज रहा है-मुझे दीखता है और एकाएक खयाल आता है कि दुमंजिला मकानों पर चढ़ने की एक उँची निसैनी उसी से टिकी हुई है। शायद, ऐसे मकानों की लम्ब-तड़ंग भीतों की रचना अभी पुराने ढंग से होती है।
सहज, जिज्ञासावश देखें, कहाँ, क्या होता है। दृश्य कौन-से, कौन से दिखाई देते हैं ! मैं उस निसैनी पर चढ़ जाता हूँ और सामनेवाली पीली ऊँची भीत के नीली फ्रेमवाले रोशनदान में से मेरी निगाहें पार निकल जाती हैं।
और, मैं स्तब्ध हो उठता हूँ।
छत से टँगे ढिलाई से गोल-गोल घूमते पंख के नीचे, दो पीली स्फटिक-सी तेज आँखें और लम्बी शलवटों भरा तंग मोतिया चेहरा है जो ठीक उन्हीं ऊँचे रोशनदानों में से, भीतर से बाहर, पार जाने के लिए ही मानो अपनी दृष्टि केन्द्रित कर रहा है। आँखों से आँखें लड़ पड़ती हैं। ध्यान से एक-दूसरे की ओर देखती हैं। स्तब्ध एकाग्र।
आश्चर्य ?
साँस के साथ शब्द निकले। ऐसी ही कोई आवाज उसने भी की होगी !
चेहरा बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है, भला आदमी मालूम होता है। पैण्ट पर शर्ट ढीली पड़ गयी है। लेकिन यह क्या !
मैं नीचे उतर पड़ता हूँ। चुपचाप रास्ता चलने लगता हूँ। कम से कम दो फर्लांग दूरी पर एक आदमी मिलता है। सिर्फ एक आदमी ! इतनी बड़ी सड़क होने पर भी लोग नहीं ! क्यों नहीं ?
पूछने पर वह शख्स कहता है, "शहर तो इस पार है, उस ओर है; वहीं कहीं इस सड़क पर बिल्डिंग का पिछवाड़ा पड़ता है। देखते नहीं हो !"
मैंने उसका चेहरा देखा ध्यान से। बायीं और दाहिनी भौंहें नाक के शुरू पर मिल गयी थीं। खुरदरा चेहरा, पंजाबी कहला सकता था। पूरा जिस्म लचकदार था। वह निःसन्देह जनाना आदमी होने की सम्भावना रखता है ! नारी तुल्य पुरुष, जिनका विकास किशोर काव्य में विशेषज्ञों का विषय है।
इतने में, मैंने उससे स्वाभाविक रूप से, अति सहज बनकर पूछा, "यह पीली बिल्डिंग कौन-सी है।" उसने मुझे पर अविश्वास करते हुए कहा, "जानते नहीं हो ? यह पागलखाना है-प्रसिद्ध पागलखाना !"
"अच्छा...!" का एक लहरदार डैश लगाकर मैं चुप हो गया और नीची निगाह किये चलने लगा।
और फिर हम दोनों के बीच दूरियाँ चौड़ी होकर गोल होने लगीं। हमारे साथ हमारे सिफर भी चलने लगे।
अपने-अपने शून्यों की खिड़कियाँ खोलकर मैंने—हम दोनों ने—एक-दूसरे की तरफ देखा कि आपस में बात कर सकते हैं या नहीं ! कि इतने में उसने मुझसे पूछा, "आप क्या काम करते हैं ?"
मैंने झेंपकर कहा, "मैं ? उठाईगिरी समझिए।"
"समझें क्यों ? जो हैं सो बताइए।"
"पता नहीं क्यों, मैं बहुत ईमानदारी की जिन्दगी जीता हूँ; झूठ नहीं बोला करता, पर स्त्री को नहीं देखता; रिश्वत नहीं लेता; भ्रष्टाचारी नहीं हूँ; दगा या फरेब नहीं करता; अलबत्ता कर्ज मुझ पर जरूर है जो मैं चुका नहीं पाता। फिर भी कमाई की रकम कर्ज में जाती है। इस पर भी मैं यह सोचता हूँ कि बुनियादी तौर से बेईमान हूँ। इसीलिए, मैंने अपने को पुलिस की जबान में उठाईगिरा कहा। मैं लेखक हूँ। अब बताइए, आप क्या हैं ?"
वह सिर्फ हँस दिया। कहा कुछ नहीं। जरा देर से उसका मुँह खुला। उसने कहा, "मैं भी आप ही हूँ।"
एकदम दबकर मैंने उससे शेकहैण्ड किया (दिल में भीतर से किसी ने कचोट लिया। हाल ही में निसैनी पर चढ़कर मैंने उस रोशनदान में से एक आदमी की सूरत देखी थी; वह चोरी नहीं तो क्या था। सन्दिग्धावस्था में उस साले ने मुझे देख लिया।)
"बड़ी अच्छी बात है। मुझे भी इस धन्धे में दिलचस्पी है, हम लेखकों का पेशा इससे कुछ मिलता जुलता है।"
इतने में भीमाकार पत्थरों की विक्टोरियन बिल्डिंग के दृश्य दूर से झलक रहे थे। हम खड़े हो गये हैं। एक बड़े-से पेड़ के नीचे पान की दूकान थी वहाँ। वहाँ एक सिलेटी रंग की औरत मिस्सी और काजल लगाये हुए बैठी हुई थी।
मेरे मुँह से अचानक निकल पड़ा, "तो यहाँ भी पान की दूकान है ?"
उसने सिर्फ इतना ही कहा, "हाँ, यहाँ भी।"
और मैं उन अधविलायती नंगी औरतों की तस्वीरें देखने लगा जो उस दूकान की शौकत को बढ़ा रही थीं।
दूकान में आईना लगा था। लहर थीं धुँधली, पीछे के मसाले के दोष से। ज्यों ही उसमें मैं अपना मुँह देखता, बिगड़ा नजर आता। कभी मोटा, लम्बा तो कभी चौड़ा। कभी नाक एकदम छोटी, तो एकदम लम्बी और मोटी ! मन में बड़ी वितृष्णा भर उठी। रास्ता लम्बा था, सूनी दुपहर। कपड़े पसीने से भीतर चिपचिया रहे थे। ऐसे मौके पर दो बातें करनेवाला आदमी मिल जाना समय और रास्ता कटने का साधन होता है।
उससे वह औरत कुछ मजाक करती रही। इतने में चार-पाँच आदमी और आ गये। वे सब घेरे खड़े रहे। चुपचाप कुछ बातें हुईं।
मैंने गौर नहीं किया। मैं इन सब बातों से दूर रहता हूँ। जो सुनाई दिया उससे यह जाहिर हुआ कि वे या तो निचले तबके में पुलिस के इनफार्मर्स हैं या ऐसे ही कुछ !
हम दोनों ने अपने-अपने और एक-दूसरे के चेहरे देखे ! दोनों खराब नजर आये। दोनों रूप बदलने लगे। दोनों हँस पड़े और यही मजाक चलता रहा।
पान खाकर हम लोग आगे बढ़े। पता नहीं क्यों मुझे अपने अनजबी साथी के जनानेपन में कोई ईश्वरीय अर्थ दिखाई दिया। जो आदमी आत्मा की आवाज दाब देता है, विवेक चेतना को घुटाले में डाल देता है। उसे क्या कहा जाए ! वैसे, वह शख्त भला मालूम होता था। फिर क्या कारण है कि उसने यह पेशा इख्तियार किया ! साहसी, हाँ, कुछ साहसिक लोग पत्रकार या गुप्तचर या ऐसे ही कुछ हो जाते हैं, अपनी आँखों में महत्त्वपूर्ण बनने के लिए, अस्तित्व की तीखी संवेदनाएँ अनुभव करने और करते रहने के लिए !
लेकिन प्रश्न यह है कि वे वैसा क्यों करते हैं ! किसी भीतरी न्यूनता के भाव पर विजय प्राप्त करने का यह एक तरीका भी हो सकता है। फिर भी, उसके दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। यही पेशा क्यों ? इसलिए, उसमें पेट और प्रवृत्ति का समन्वय है ! जो हो, इस शख्त का जनानापन खास मानी रखता है।
हमने वह रास्ता पार कर लिया और अब हम फिर से फैशनेबल रास्ते पर आ गये, जिसके दोनों ओर युकलिप्टस के पेड़ कतार बाँधे खड़े थे। मैंने पूछा, "यह रास्ता कहाँ जाता है ? उसने कहा, "पागलखाने की ओर।" मैं जाने क्यों सन्नाटे में आ गया।
विषय बदलने के लिए मैने कहा, "तुम यह धन्धा कब से कर रहे हो ?"
उसने मेरी तरफ इस तरह देखा मानो यह सवाल उसे नागवार गुजरा हो।
मैं कुछ नहीं बोला। चुपचाप चला, चलता रहा। लगभग पाँच मिनट बाद जब हम उस भैरों के गेरुए, सुनहले, पन्नी जड़े पत्थर तक पहुँच गये, जो इस अत्याधिक युग में एक तार के खन्भे के पास श्रद्धापूर्वक स्थापित किया गया था, उसने "कहा मेरा किस्सा मुख्तसर है। लार्ज शरम दिखावे की चीजें हैं। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए कह रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़े करोड़पति सेठ का लड़का हूँ। उनके घर में जो काम करनेवालियाँ हुआ करती थीं, उनमें से एक मेरी माँ है, जो अभी भी वहीं है। मैं, घर से दूर, पाला-पोसा गया, मेरे पिता के खर्चे से ! माँ पिलाने आती। उसी के कहने से मैंने बमुश्किल तमाम मैट्रिक किया। फिर, किसी सिफारिश से सी.आई.डी. की ट्रेनिंग में चला गया। तबसे यही काम कर रहा हूँ। बाद में पता चला कि वहाँ का खर्च भी वही सेठ देता है। उसका हाथ मुझ पर अभी तक है। तुम उठाईगिरे हो, इसलिए कहा ! अरे ! वैसें तो तुम लेखक-वेखक भी हो। बहुत से लेखक और पत्रकार इनफॉर्मर हैं ! तो इसलिए मैंने सोचा, चलो अच्छा हुआ। एक साथी मिल गया।"
उस आदमी में मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ गयी। डर भी लगा। घृणा भी हुई। किस आदमी से पाला पड़ा। फिर भी, उस अहाते पर चढ़कर मैं झाँक चुका था इसलिए एक अनदिखती जंजीर से बँध तो गया ही था।
उस जनाने ने कहना जारी रखा, "उस पागलखाने में कई ऐसे लोग डाल दिये गये हैं जो सचमुच आज की निगाह से बड़े पागल हैं। लेकिन उन्हें पागल कहने की इच्छा रखने के लिए आज की निगाह होना जरूरी है।"
मैंने उकसाते हुए कहा, "आज की निगाह से क्या मतलब ?"
उसने भौंहें समेट लीं। मेरी आँखों में आँखें डालकर उसने कहना शुरू किया, "जो आदमी आत्मा की आवाज कभी कभी सुन लिया करता है और उसे बयान करके उसने छुट्टी पा लेता है, वह लेखक हो जाता है। आत्मा की आवाज को लगातार सुनता है, और कहता कुछ नहीं, वह भोला भाला सीधा-सादा बेवकूफ है। जो उसकी आवाज बहुत ज्यादा सुना करता है और वैसा करने लगता है, वह समाज विरोधी तत्त्वों में यों ही शामिल हो जाया करता है। लेकिन जो आदी आत्मा की आवाज जरूरत से ज्यादा सुन करके हमेशा बेचैन रहा करता है और उस बेचैनी में भीतर के हुक्म का पालन करता है, वह निहायत पागल है। पुराने जमाने में सन्त हो सकता था। आजकल उसे पागलखाने में डाल दिया जाता है।"
मुझे शक हुआ कि मैं किसी फैण्टेसी में रह रहा हूँ। यह कोई ऐसा वैसा कोई गुप्तचर नहीं है। या तो यह खुद पागल है या कोई पहुँचा हुआ आदमी है ! लेकिन वह पागल भी नहीं है न वह पहुँचा हुआ है। वह तो सिर्फ जनाना आदमी है या वैज्ञानिक शब्दावली प्रयोग करूँ तो यह कहना होगा कि वह है तो जवान पट्ठा लेकिन उसमें जो लचक है वह औरत के चलने की याद दिलाती है!
मैंने उसे पूछा, "तुमने कहीं ट्रेनिंग पायी है ?"
"सिर्फ तजुर्बे से सीखा है ! मुझे इनाम भी मिला है।"
मैंने कहा, "अच्छा !"
मैं सड़क पार कर लेता हूँ। जंगली, बेमहक लेकिन खूबसूरत विदेशी फूलों के नीचे ठहर-सा जाता हूँ कि जो फूल, भीत के पासवाले अहाते की आदमकद दीवार के ऊपर फैले सड़क के बाजू पर बाँहें बिछाकर झुक गये हैं। पता नहीं कैसे, किस साहस से व क्यों उसी अहाते के पास बिजली का ऊँचा खम्भा—जो पाँच-छह दिशाओं में जानेवाली सूनी सड़कों पर तारों की सीधी लकीरें भेज रहा है-मुझे दीखता है और एकाएक खयाल आता है कि दुमंजिला मकानों पर चढ़ने की एक उँची निसैनी उसी से टिकी हुई है। शायद, ऐसे मकानों की लम्ब-तड़ंग भीतों की रचना अभी पुराने ढंग से होती है।
सहज, जिज्ञासावश देखें, कहाँ, क्या होता है। दृश्य कौन-से, कौन से दिखाई देते हैं ! मैं उस निसैनी पर चढ़ जाता हूँ और सामनेवाली पीली ऊँची भीत के नीली फ्रेमवाले रोशनदान में से मेरी निगाहें पार निकल जाती हैं।
और, मैं स्तब्ध हो उठता हूँ।
छत से टँगे ढिलाई से गोल-गोल घूमते पंख के नीचे, दो पीली स्फटिक-सी तेज आँखें और लम्बी शलवटों भरा तंग मोतिया चेहरा है जो ठीक उन्हीं ऊँचे रोशनदानों में से, भीतर से बाहर, पार जाने के लिए ही मानो अपनी दृष्टि केन्द्रित कर रहा है। आँखों से आँखें लड़ पड़ती हैं। ध्यान से एक-दूसरे की ओर देखती हैं। स्तब्ध एकाग्र।
आश्चर्य ?
साँस के साथ शब्द निकले। ऐसी ही कोई आवाज उसने भी की होगी !
चेहरा बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है, भला आदमी मालूम होता है। पैण्ट पर शर्ट ढीली पड़ गयी है। लेकिन यह क्या !
मैं नीचे उतर पड़ता हूँ। चुपचाप रास्ता चलने लगता हूँ। कम से कम दो फर्लांग दूरी पर एक आदमी मिलता है। सिर्फ एक आदमी ! इतनी बड़ी सड़क होने पर भी लोग नहीं ! क्यों नहीं ?
पूछने पर वह शख्स कहता है, "शहर तो इस पार है, उस ओर है; वहीं कहीं इस सड़क पर बिल्डिंग का पिछवाड़ा पड़ता है। देखते नहीं हो !"
मैंने उसका चेहरा देखा ध्यान से। बायीं और दाहिनी भौंहें नाक के शुरू पर मिल गयी थीं। खुरदरा चेहरा, पंजाबी कहला सकता था। पूरा जिस्म लचकदार था। वह निःसन्देह जनाना आदमी होने की सम्भावना रखता है ! नारी तुल्य पुरुष, जिनका विकास किशोर काव्य में विशेषज्ञों का विषय है।
इतने में, मैंने उससे स्वाभाविक रूप से, अति सहज बनकर पूछा, "यह पीली बिल्डिंग कौन-सी है।" उसने मुझे पर अविश्वास करते हुए कहा, "जानते नहीं हो ? यह पागलखाना है-प्रसिद्ध पागलखाना !"
"अच्छा...!" का एक लहरदार डैश लगाकर मैं चुप हो गया और नीची निगाह किये चलने लगा।
और फिर हम दोनों के बीच दूरियाँ चौड़ी होकर गोल होने लगीं। हमारे साथ हमारे सिफर भी चलने लगे।
अपने-अपने शून्यों की खिड़कियाँ खोलकर मैंने—हम दोनों ने—एक-दूसरे की तरफ देखा कि आपस में बात कर सकते हैं या नहीं ! कि इतने में उसने मुझसे पूछा, "आप क्या काम करते हैं ?"
मैंने झेंपकर कहा, "मैं ? उठाईगिरी समझिए।"
"समझें क्यों ? जो हैं सो बताइए।"
"पता नहीं क्यों, मैं बहुत ईमानदारी की जिन्दगी जीता हूँ; झूठ नहीं बोला करता, पर स्त्री को नहीं देखता; रिश्वत नहीं लेता; भ्रष्टाचारी नहीं हूँ; दगा या फरेब नहीं करता; अलबत्ता कर्ज मुझ पर जरूर है जो मैं चुका नहीं पाता। फिर भी कमाई की रकम कर्ज में जाती है। इस पर भी मैं यह सोचता हूँ कि बुनियादी तौर से बेईमान हूँ। इसीलिए, मैंने अपने को पुलिस की जबान में उठाईगिरा कहा। मैं लेखक हूँ। अब बताइए, आप क्या हैं ?"
वह सिर्फ हँस दिया। कहा कुछ नहीं। जरा देर से उसका मुँह खुला। उसने कहा, "मैं भी आप ही हूँ।"
एकदम दबकर मैंने उससे शेकहैण्ड किया (दिल में भीतर से किसी ने कचोट लिया। हाल ही में निसैनी पर चढ़कर मैंने उस रोशनदान में से एक आदमी की सूरत देखी थी; वह चोरी नहीं तो क्या था। सन्दिग्धावस्था में उस साले ने मुझे देख लिया।)
"बड़ी अच्छी बात है। मुझे भी इस धन्धे में दिलचस्पी है, हम लेखकों का पेशा इससे कुछ मिलता जुलता है।"
इतने में भीमाकार पत्थरों की विक्टोरियन बिल्डिंग के दृश्य दूर से झलक रहे थे। हम खड़े हो गये हैं। एक बड़े-से पेड़ के नीचे पान की दूकान थी वहाँ। वहाँ एक सिलेटी रंग की औरत मिस्सी और काजल लगाये हुए बैठी हुई थी।
मेरे मुँह से अचानक निकल पड़ा, "तो यहाँ भी पान की दूकान है ?"
उसने सिर्फ इतना ही कहा, "हाँ, यहाँ भी।"
और मैं उन अधविलायती नंगी औरतों की तस्वीरें देखने लगा जो उस दूकान की शौकत को बढ़ा रही थीं।
दूकान में आईना लगा था। लहर थीं धुँधली, पीछे के मसाले के दोष से। ज्यों ही उसमें मैं अपना मुँह देखता, बिगड़ा नजर आता। कभी मोटा, लम्बा तो कभी चौड़ा। कभी नाक एकदम छोटी, तो एकदम लम्बी और मोटी ! मन में बड़ी वितृष्णा भर उठी। रास्ता लम्बा था, सूनी दुपहर। कपड़े पसीने से भीतर चिपचिया रहे थे। ऐसे मौके पर दो बातें करनेवाला आदमी मिल जाना समय और रास्ता कटने का साधन होता है।
उससे वह औरत कुछ मजाक करती रही। इतने में चार-पाँच आदमी और आ गये। वे सब घेरे खड़े रहे। चुपचाप कुछ बातें हुईं।
मैंने गौर नहीं किया। मैं इन सब बातों से दूर रहता हूँ। जो सुनाई दिया उससे यह जाहिर हुआ कि वे या तो निचले तबके में पुलिस के इनफार्मर्स हैं या ऐसे ही कुछ !
हम दोनों ने अपने-अपने और एक-दूसरे के चेहरे देखे ! दोनों खराब नजर आये। दोनों रूप बदलने लगे। दोनों हँस पड़े और यही मजाक चलता रहा।
पान खाकर हम लोग आगे बढ़े। पता नहीं क्यों मुझे अपने अनजबी साथी के जनानेपन में कोई ईश्वरीय अर्थ दिखाई दिया। जो आदमी आत्मा की आवाज दाब देता है, विवेक चेतना को घुटाले में डाल देता है। उसे क्या कहा जाए ! वैसे, वह शख्त भला मालूम होता था। फिर क्या कारण है कि उसने यह पेशा इख्तियार किया ! साहसी, हाँ, कुछ साहसिक लोग पत्रकार या गुप्तचर या ऐसे ही कुछ हो जाते हैं, अपनी आँखों में महत्त्वपूर्ण बनने के लिए, अस्तित्व की तीखी संवेदनाएँ अनुभव करने और करते रहने के लिए !
लेकिन प्रश्न यह है कि वे वैसा क्यों करते हैं ! किसी भीतरी न्यूनता के भाव पर विजय प्राप्त करने का यह एक तरीका भी हो सकता है। फिर भी, उसके दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। यही पेशा क्यों ? इसलिए, उसमें पेट और प्रवृत्ति का समन्वय है ! जो हो, इस शख्त का जनानापन खास मानी रखता है।
हमने वह रास्ता पार कर लिया और अब हम फिर से फैशनेबल रास्ते पर आ गये, जिसके दोनों ओर युकलिप्टस के पेड़ कतार बाँधे खड़े थे। मैंने पूछा, "यह रास्ता कहाँ जाता है ? उसने कहा, "पागलखाने की ओर।" मैं जाने क्यों सन्नाटे में आ गया।
विषय बदलने के लिए मैने कहा, "तुम यह धन्धा कब से कर रहे हो ?"
उसने मेरी तरफ इस तरह देखा मानो यह सवाल उसे नागवार गुजरा हो।
मैं कुछ नहीं बोला। चुपचाप चला, चलता रहा। लगभग पाँच मिनट बाद जब हम उस भैरों के गेरुए, सुनहले, पन्नी जड़े पत्थर तक पहुँच गये, जो इस अत्याधिक युग में एक तार के खन्भे के पास श्रद्धापूर्वक स्थापित किया गया था, उसने "कहा मेरा किस्सा मुख्तसर है। लार्ज शरम दिखावे की चीजें हैं। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए कह रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़े करोड़पति सेठ का लड़का हूँ। उनके घर में जो काम करनेवालियाँ हुआ करती थीं, उनमें से एक मेरी माँ है, जो अभी भी वहीं है। मैं, घर से दूर, पाला-पोसा गया, मेरे पिता के खर्चे से ! माँ पिलाने आती। उसी के कहने से मैंने बमुश्किल तमाम मैट्रिक किया। फिर, किसी सिफारिश से सी.आई.डी. की ट्रेनिंग में चला गया। तबसे यही काम कर रहा हूँ। बाद में पता चला कि वहाँ का खर्च भी वही सेठ देता है। उसका हाथ मुझ पर अभी तक है। तुम उठाईगिरे हो, इसलिए कहा ! अरे ! वैसें तो तुम लेखक-वेखक भी हो। बहुत से लेखक और पत्रकार इनफॉर्मर हैं ! तो इसलिए मैंने सोचा, चलो अच्छा हुआ। एक साथी मिल गया।"
उस आदमी में मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ गयी। डर भी लगा। घृणा भी हुई। किस आदमी से पाला पड़ा। फिर भी, उस अहाते पर चढ़कर मैं झाँक चुका था इसलिए एक अनदिखती जंजीर से बँध तो गया ही था।
उस जनाने ने कहना जारी रखा, "उस पागलखाने में कई ऐसे लोग डाल दिये गये हैं जो सचमुच आज की निगाह से बड़े पागल हैं। लेकिन उन्हें पागल कहने की इच्छा रखने के लिए आज की निगाह होना जरूरी है।"
मैंने उकसाते हुए कहा, "आज की निगाह से क्या मतलब ?"
उसने भौंहें समेट लीं। मेरी आँखों में आँखें डालकर उसने कहना शुरू किया, "जो आदमी आत्मा की आवाज कभी कभी सुन लिया करता है और उसे बयान करके उसने छुट्टी पा लेता है, वह लेखक हो जाता है। आत्मा की आवाज को लगातार सुनता है, और कहता कुछ नहीं, वह भोला भाला सीधा-सादा बेवकूफ है। जो उसकी आवाज बहुत ज्यादा सुना करता है और वैसा करने लगता है, वह समाज विरोधी तत्त्वों में यों ही शामिल हो जाया करता है। लेकिन जो आदी आत्मा की आवाज जरूरत से ज्यादा सुन करके हमेशा बेचैन रहा करता है और उस बेचैनी में भीतर के हुक्म का पालन करता है, वह निहायत पागल है। पुराने जमाने में सन्त हो सकता था। आजकल उसे पागलखाने में डाल दिया जाता है।"
मुझे शक हुआ कि मैं किसी फैण्टेसी में रह रहा हूँ। यह कोई ऐसा वैसा कोई गुप्तचर नहीं है। या तो यह खुद पागल है या कोई पहुँचा हुआ आदमी है ! लेकिन वह पागल भी नहीं है न वह पहुँचा हुआ है। वह तो सिर्फ जनाना आदमी है या वैज्ञानिक शब्दावली प्रयोग करूँ तो यह कहना होगा कि वह है तो जवान पट्ठा लेकिन उसमें जो लचक है वह औरत के चलने की याद दिलाती है!
मैंने उसे पूछा, "तुमने कहीं ट्रेनिंग पायी है ?"
"सिर्फ तजुर्बे से सीखा है ! मुझे इनाम भी मिला है।"
मैंने कहा, "अच्छा !"
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book