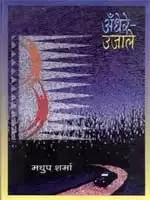|
नारी विमर्श >> अँधेरे उजाले अँधेरे उजालेमधुप शर्मा
|
438 पाठक हैं |
||||||
उपन्यास न केवल गहरे में उद्वेलित करता है, झकझोरता है, बल्कि बार-बार सोचने पर भी बाध्य करता है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
उपन्यास न केवल गहरे में उद्वेलित करता है, झकझोरता है, बल्कि बार-बार
सोचने पर भी बाध्य करता है।
...प्रसंग इतने सजीव और विश्वसनीय उभरे हैं कि जीवन से जुड़ने वाला, दिल में गहरा दर्द रखने वाला व्यक्ति ही उन्हें कलम पर ला सकता है।...परन्तु ऐसी शोचनीय स्थिति में भी, मानवीय मूल्यों में लेखक की आस्था बराबर बनी हुई है। मानव ह्रदय में सद्भावना के सोते बिलकुल सूख नहीं गये हैं। उपन्यास में अनेक ऐसे पात्र हैं जो अपह्रत, उत्पीड़ित व्यक्तियों को सहारा देते हैं, जीवन में उनका संबल बनते हैं, उन्हें न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं।
...प्रसंग इतने सजीव और विश्वसनीय उभरे हैं कि जीवन से जुड़ने वाला, दिल में गहरा दर्द रखने वाला व्यक्ति ही उन्हें कलम पर ला सकता है।...परन्तु ऐसी शोचनीय स्थिति में भी, मानवीय मूल्यों में लेखक की आस्था बराबर बनी हुई है। मानव ह्रदय में सद्भावना के सोते बिलकुल सूख नहीं गये हैं। उपन्यास में अनेक ऐसे पात्र हैं जो अपह्रत, उत्पीड़ित व्यक्तियों को सहारा देते हैं, जीवन में उनका संबल बनते हैं, उन्हें न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं।
अँधेरे-उजाले
मुझे मधुप शर्मा जी के उपन्यास ‘अँधेरे-उजाले’ को
पढ़ने का सुअवसर मिला है। उपन्यास न केवल गहरे में उद्वेलित करता है,
झकझोरता है, बल्कि बार-बार सोचने पर भी बाध्य करता है। मैं नहीं जानता,
उपन्यास का ताना-बाना बुनने के लिए प्रसंग, कहाँ तक वास्तविक जीवन से उठाए
गए हैं और कहाँ तक कल्पना की देन हैं, पर वे इतने सजीव और विश्वसनीय बनकर
उभरे हैं कि जीवन से जुड़ने वाला, दिल में गहरा दर्द रखने वाला व्यक्ति ही
उन्हें क़लम पर ला सकता है।
यह यथार्थ बहुआयामी है। एक ओर हमारी परम्परागत रूढ़ प्रथाएँ, कुरीतियाँ और अंधविश्वास, अभी भी हमें अपनी जकड़ में लिए हुए हैं, दूसरी ओर आधुनिकता के नाम पर आज हमारे समाज में बढ़ती उच्छृंखलता, हृदयहीनता, लम्पटता और भयावह रूप में बढ़ता स्वार्थ, सभी मानवीय मूल्यों को रौंदता हुआ, मात्र स्वार्थ सिद्धि को अपना लक्ष्य बनाए हुए है। ऐसे क्रूर माहौल में केवल निर्दोष, निश्छल व्यक्ति ही पिसते हैं, भले ही वह दादा की विधवा बहन हो, भोली-भाली कॉलिज की छात्रा हो या मुकुट बिहारी हो।
स्थिति की विडम्बना इस बात में है कि यह सब एक ऐसे देश में हो रहा है जिसकी प्राचीन संस्कृति और नैतिक मान्यताएँ, संसार-भर के लिए प्रकाश-स्तम्भ के समान रही हैं।
कभी-कभी निराशा का घटाटोप इतना अंधकारमय हो जाता है कि स्वयं लेखक के शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति हँसता है तो ‘‘अपना दुःख-दर्द छिपाने के लिए। यह हँसी का वरदान ईश्वर ने एक बहुत ही ख़ूबसूरत आवरण के रूप में दिया है, वरना पता नहीं मानव की यह दुनिया कितनी कुरूप और भयानक दिखती...।’’
परन्तु ऐसी शोचनीय स्थिति में भी, मानवीय मूल्यों में लेखक की आस्था बराबर बनी हुई है। मानव हृदय में सद्भावना के सोते बिलकुल सूख नहीं गए हैं। उपन्यास में अनेक ऐसे पात्र हैं जो अपहृत, उत्पीड़ित व्यक्तियों को सहारा देते हैं, जीवन में उनका सम्बल बनते हैं, उन्हें न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं, लेखक की दृष्टि अनुसार करुणा, सद्भावना, सहृदयता, सहयोग की भावनाओं को जगाते हुए, स्वार्थपरता से आक्रांत इस माहौल में भी मानवीयता को बनाए रखने में हम सहायक हो सकते हैं।
और यहीं पर वृद्धाश्रम एक प्रतीक बनकर सामने आता है। जीवन-प्रवाह में से एक तरह से बाहर फेंके हुए लोग, इसी चेतना से उत्प्रेरित, एक-दूसरे का हाथ थामे, आपस में सहयोग करते हुए, साँझे प्रयास करते हुए, अपने जीवन में सुखी और सार्थक बना पाते हैं।
मधुप जी की क़लम से और भी अनेक रोचक, सारगर्भित रचनाओं की अपेक्षा बनी रहेगी।
यह यथार्थ बहुआयामी है। एक ओर हमारी परम्परागत रूढ़ प्रथाएँ, कुरीतियाँ और अंधविश्वास, अभी भी हमें अपनी जकड़ में लिए हुए हैं, दूसरी ओर आधुनिकता के नाम पर आज हमारे समाज में बढ़ती उच्छृंखलता, हृदयहीनता, लम्पटता और भयावह रूप में बढ़ता स्वार्थ, सभी मानवीय मूल्यों को रौंदता हुआ, मात्र स्वार्थ सिद्धि को अपना लक्ष्य बनाए हुए है। ऐसे क्रूर माहौल में केवल निर्दोष, निश्छल व्यक्ति ही पिसते हैं, भले ही वह दादा की विधवा बहन हो, भोली-भाली कॉलिज की छात्रा हो या मुकुट बिहारी हो।
स्थिति की विडम्बना इस बात में है कि यह सब एक ऐसे देश में हो रहा है जिसकी प्राचीन संस्कृति और नैतिक मान्यताएँ, संसार-भर के लिए प्रकाश-स्तम्भ के समान रही हैं।
कभी-कभी निराशा का घटाटोप इतना अंधकारमय हो जाता है कि स्वयं लेखक के शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति हँसता है तो ‘‘अपना दुःख-दर्द छिपाने के लिए। यह हँसी का वरदान ईश्वर ने एक बहुत ही ख़ूबसूरत आवरण के रूप में दिया है, वरना पता नहीं मानव की यह दुनिया कितनी कुरूप और भयानक दिखती...।’’
परन्तु ऐसी शोचनीय स्थिति में भी, मानवीय मूल्यों में लेखक की आस्था बराबर बनी हुई है। मानव हृदय में सद्भावना के सोते बिलकुल सूख नहीं गए हैं। उपन्यास में अनेक ऐसे पात्र हैं जो अपहृत, उत्पीड़ित व्यक्तियों को सहारा देते हैं, जीवन में उनका सम्बल बनते हैं, उन्हें न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं, लेखक की दृष्टि अनुसार करुणा, सद्भावना, सहृदयता, सहयोग की भावनाओं को जगाते हुए, स्वार्थपरता से आक्रांत इस माहौल में भी मानवीयता को बनाए रखने में हम सहायक हो सकते हैं।
और यहीं पर वृद्धाश्रम एक प्रतीक बनकर सामने आता है। जीवन-प्रवाह में से एक तरह से बाहर फेंके हुए लोग, इसी चेतना से उत्प्रेरित, एक-दूसरे का हाथ थामे, आपस में सहयोग करते हुए, साँझे प्रयास करते हुए, अपने जीवन में सुखी और सार्थक बना पाते हैं।
मधुप जी की क़लम से और भी अनेक रोचक, सारगर्भित रचनाओं की अपेक्षा बनी रहेगी।
-भीष्म साहनी
एक उपलब्धि
कहाँ श्री भीष्म साहनी, साहित्य में एक क़द्दावर प्रतिष्ठित नाम
और कहाँ मैं, अपेक्षाकृत नया और अनजाना। उनसे मिला भी तो सिर्फ़ एक ही बार
था, वो भी वर्षों पहले उनके अग्रज बलराज जी के घर। इसलिए काफ़ी संकोच के
बाद ही, नवम्बर के पहले सप्ताह में मैं उन्हें लिख पाया था-मैं जानता हूँ
आप बहुत व्यस्त हैं। थोड़ा समय निकालकर मेरा अगला उपन्यास
‘अँधेरे-उजाले’ आप पढ़ सकें और भूमिका के रूप में कुछ
लिख भी दें तो उसे अपना सौभाग्य समझूँगा। जवाब आया-दिसम्बर में मुझे दो
बार दिल्ली से बाहर जाना है। पाण्डुलिपि जल्दी भेज दें तो निर्विघ्न पढ़
लूँगा। लेकिन डाक विभाग के सौजन्य से उनका वो पत्र मुझे बारह दिन बाद
मिला। हिसाब लगाया तो पहली दिसम्बर से पहले पाण्डुलिपि का पहुँचना असंभव
था। मैंने फ़ोन किया। बोले, 10 दिसम्बर को मैं पुणे पहुँच रहा हूँ। तब
पाण्डुलिपि निम्नलिखित पते पर पहुँच जाए तो उसे पढ़कर ही मैं अपने काम पर
बैठूँगा। मैंने पाण्डुलिपि भेज दी, पर दिल्ली में व्यस्तता के कारण उनका
पुणे आना 16 दिसम्बर तक टल गया।
आज अचानक उनका 26 दिसम्बर का लिखा हुआ पत्र और साथ में भूमिका पाकर मैं इतना भावविभोर हो उठा हूँ कि छलकते हुए आँसुओं को रोक नहीं पाया। ये आँसू उनसे मिले प्यार और अपनेपन की खुशी के हैं या उनसे पाए प्रोत्साहन और प्रशंसा के, या उनके प्रति मेरी श्रद्धा के, या सब मिले-जुले, मैं ख़ुद भी कहाँ जान पा रहा हूँ।
‘अँधेरे-उजाले’ पर उनकी प्रतिक्रिया आप पढ़ ही चुके हैं, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मेरी कृति के साथ उनके नाम का जुड़ना, मेरे लिए एक बड़ी भारी उपलब्धि है।
पाठकों से भी मैं अपनापन और प्यार पा सकूँगा, यही आशा है।
आज अचानक उनका 26 दिसम्बर का लिखा हुआ पत्र और साथ में भूमिका पाकर मैं इतना भावविभोर हो उठा हूँ कि छलकते हुए आँसुओं को रोक नहीं पाया। ये आँसू उनसे मिले प्यार और अपनेपन की खुशी के हैं या उनसे पाए प्रोत्साहन और प्रशंसा के, या उनके प्रति मेरी श्रद्धा के, या सब मिले-जुले, मैं ख़ुद भी कहाँ जान पा रहा हूँ।
‘अँधेरे-उजाले’ पर उनकी प्रतिक्रिया आप पढ़ ही चुके हैं, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मेरी कृति के साथ उनके नाम का जुड़ना, मेरे लिए एक बड़ी भारी उपलब्धि है।
पाठकों से भी मैं अपनापन और प्यार पा सकूँगा, यही आशा है।
-मधुप शर्मा
मुकुट बिहारी से मेरी मुलाक़ात को आप संयोग कहें या इत्तफ़ाक़िया या
आकस्मिक कहकर टाल दें, लेकिन मुझे ये तमाम समानधर्मी और समानार्थी शब्द
अधूरे से लगते हैं। तनिक भी सोचता हूँ तो साफ़ दिखाई देने लगता है कि उस
दिन...। उस दिन मेरे न चाहते हुए भी, किसी अनजानी परोक्ष शक्ति ने बरबस ही
मुझे धकियाते धकेलते उसके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया था, अपनी ही किसी
योजना के अनुसार। भई संयोग होता है तो कभी-कभार, एक-आध बार, पर अगर सुबह
से शाम तक कुछ अप्रत्याशित और अनापेक्षिक घटनाओं का सिलसिला जारी रहे तो
उसे आप क्या कहेंगे ?
ख़ैर, बात पूरी सुना दूँ तो आप ख़ुद ही फ़ैसला कीजिएगा।
उस दिन सब से पहली बात तो यह हुई कि नाश्ता करने बैठा ही था जब टेलीफ़ोन की घंटी घनघनाई। चम्मच की जगह चोग़ा उठाया। बिटिया की आवाज़ थी, ‘‘शहर चलते हैं क्या ?’’
कुछ अचंभा सा हुआ था। कहा, ‘‘काम तो कोई है नहीं। क्या करूँगा जाकर ? व्यर्थ की थकावट....साढ़े तीन-चार घंटे का आना-जाना और...’’
‘‘ठीक है। मैंने तो यूँ ही पूछा। बहुत दिनों से कहीं आए-गए नहीं न आप। घर में बैठे-बैठे....’’
‘‘आज तो रहने ही दो।’’ एक तरह से उसी के शब्द मेरी ज़बान पर आ गए थे, अनचाहे।
उन लोगों का शहर आना-जाना तो लगा ही रहता है। रोज़ नहीं तो हफ़्ते में कम-से-कम तीन-चार दिन। कभी वो, कभी उसके पतिदेव, या कभी दोनों। मैंने उसे अकेली जाते देख एक बार पूछा, ‘‘चलूँ तुम्हारे साथ ?’’ तो उसका जवाब था, ‘‘नहीं-नहीं, बहुत थक जाएँगे आप। ट्रैफ़िक इतना बढ़ गया है कि जगह-जगह ट्रैफ़िक जाम। बैठे-बैठे उकताहट होने लगती है। कार का सफ़र भी अब आनंददायक नहीं, एक मजबूरी है। वैसे आप को कुछ काम है शहर में ? मुझे बताइए, मैं करती आऊँगी।’’
‘‘नहीं-नहीं, काम कोई नहीं। वो तो तुम अकेली...’’
‘‘ओह दादा...आप भी बस...अब मैं बड़ी हो गई हूँ, और वैसे भी मेरी फ़िक्र करने वाला अब यह है न।’’
उसने अपने पति की ओर इशारा किया था। दोनों मुस्कराए थे। बिटिया ने जोड़ा था, ‘‘आज भी मैं अकेली नहीं जा रही। ड्राइवर है मेरे साथ।’’
टेलीफ़ोन रख के मैं नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद एक अजीब सा अहसास हुआ। सारा घर जैसे घुटन से भर गया है। गर्मी और उमस बढ़ती जा रही है।...हवा एकदम बंद। मेरी निगाहें छत की तरफ़ उठीं। पंखा तो चल रहा था। मैंने उठकर रफ़्तार तेज़ कर दी। लेकिन घुटन और उमस में कोई फ़र्क नहीं हुआ।...कुछ अजीब सी बेचैनी, जो बढ़ती ही जा रही थी।
मैंने नाश्ता बीच में ही छोड़कर फ़ोन पर नम्बर घुमाया। कुछ देर बाद कहा था, ‘‘ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कितने बजे निकलेंगे ?’’
‘‘मुंबई का कार्यक्रम तो आज का रद्द हो गया, दादा। अब शायद सोम या मंगल को जाएँ।’’
‘‘अच्छा !’’
‘‘वैसे मैं सांताक्रूज़ तक जा रही हूँ। आप ड्राइव के तौर पर चलना चाहें तो...’’
‘‘किस समय ?’’
‘‘यही...कोई ग्यारह बजे।’’
‘‘ठीक है, मैं तैयार रहूँगा।’’
लगा जैसे ज़बरदस्ती ही उगलवाया हो वो वाक्य किसी ने मुझसे। भीतर-ही-भीतर एक द्वन्द्व सा चलता रहा था कुछ देर। अपने ही अन्दर से एक आवाज़ सुनाई दी थी, ‘अब सांताक्रूज़ में क्या काम है तुम्हें जो झट तैयार हो गए ?’
‘हो गया तैयार तो तुम्हें क्या ?’’
‘‘नहीं-नहीं, मुझे क्या। तुम्हीं कहा करते हो, बिना काम के कहीं जाने का क्या मतलब अब थकोगे नहीं ?’’
‘ओहो तुम भी...’’
‘‘तुम तो बुरा मान गए दोस्त। अपना समझता हूँ इसीलिए कहा। अब इतना क्यों सोच रहे हो ? चाहो तो अब भी फ़ोन उठाओ और मना कर दो।’
‘नहीं, नहीं, नहीं। नहीं करूँगा मना। मुझे जाना है तो बस जाना है। चुप रहो तुम।’
‘ह...ह...ह’
कुछ देर बाद मुझे लगा था, यह बच्चे की-सी ज़िद क्यूँ ? कौन-सी ऐसी मजबूरी है जो आज स्वभाव के विपरीत मुझे इस दुविधा में डाले हुए है ? इतनी साधारण-सी बात पर इतना डाँवाडोल तो कभी नहीं पाया था मैंने अपने आप को। मेरी तो हर बात सीधी-सपाट हुआ करती है हमेशा। दो टूक, इधर या उधर। लेकिन आ तमाम क्रियाएँ जैसे मैं नहीं कर रहा, कोई और करवा रहा है मुझसे।
रास्ते में मैंने आरती से पूछा, ‘‘मुंबई जाते-जाते सांताक्रूज़ का प्रोग्राम कैसे बन गया ?’’
‘‘मुबंई का कार्यक्रम तो सिर्फ़ मुल्तवी हुआ है। पहले सोचा था शाम को लौटते हुए थोड़ी देर सांताक्रूज़ रुक लूँगी। वो अपनी ज्योत्सना है न, टाइपिस्ट, कितने ही दिनों से कह रही थी, उसका कोई रिश्तेदार है। बेचारों के पास मकान तो हैं छोटा-सा, एक कमरे का, और रहने वाले हैं पाँच। गाँव से बूढ़ी माँ को भी लाना पड़ा, जिसे अब वे वृद्धाश्रम में रखना चाहते हैं। मेरी वहाँ पहचान है, इसलिए...।’’
वृद्धाश्रम की बात से ज़रूर मेरे चेहरे पर कुछ बदलाव आया होगा, जिसे महसूसते हुए आरती ने क्षमा-याचना के से स्वर में तुरन्त ही कहा, ‘‘मुझे बिलकुल याद नहीं रहा कि वृद्धाश्रम में जाना आपको अच्छा नहीं लगता। ख़ैर, जुहू का एक चक्कर लगा के लौट चलते हैं। आश्रम में मैं फिर कभी हो आऊँगी, कल-वल।’’
‘‘नहीं-नहीं, तुम जिस काम के लिए निकली हो उसे कर ही डालो। मैं कार में बैठा रहूँगा।’’
‘‘पक्का ?’’
‘‘बिल्कुल पक्का ।’’
‘‘पिछली बार की तरह न हो। हफ़्ता-भर तक आपकी उदासी नहीं टूटी थी। हर समय वही सोच, वही बात।...वही माहौल छाया रहा था दिलो-दिमाग़ पर आपके।’’
‘‘वो तो बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, आरती। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के साथ वही होता जो मेरे साथ हुआ। अब तुम भी कभी बालाश्रम में खाना और मिठाई लेकर जाती हो, कभी वृद्धों के लिए वस्त्र इकट्ठे करती हो, चीनी-चावल दे आती हो, यह भी तुम्हारी संवेदनशीलता का ही सक्रियात्मक रूप है।...और यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि वहाँ जाना मुझे अच्छा नहीं लगा था। हाँ, दुःख ज़रूर हुआ था उन्हें देखकर। एक उदास, उजाड़-सा माहौल। मुर्झाए हुए चेहरे, धँसी हुई आँखें, झुके हुए माथे, मजबूरी और लाचारी की मुजस्सम तस्वीरें। कुछ खोजती हुई, कुछ पूछती हुई-सी उनकी पनीली निगाहें। अपनों से कटे हुए दूर। अपने आप को तिलतिल करके मिटता हुआ देखने के लिए विवश, जैसे कण-कण करके चुकते हुए तेल और तिलतिल करके जलती हुई बाती का साक्षी मिट्टी का दिया। बुढ़ापा तो ज़िन्दगी की ही नौ अवस्थाओं में से एक है, फिर इतना उपेक्षित क्यूँ ? क्या इसीलिए कि उसकी उपयोगिता कम हो गई है, या बिलकुल नहीं रही ?...हमने तो संयुक्त परिवारों का दौर भी देखा है आरती, जहाँ बुढ़ापे की अहमियत और बढ़ जाती थी। परिवार की कोई भी समस्या हो, राय-मशविरे और हल के लिए निगाहें बुजुर्गों की तरफ़ ही उठती थीं। उन्हें अनुभव का ख़ज़ाना और उनके शब्दों को जीवन का निचोड़ समझा जाता था।...पर अब ज़माना बहुत बदल गया है। बल्कि बदलता ही चला जा रहा है, हर रोज़, बड़ी तेज़ी के साथ।...टूटते हुए परिवार, विखंडित होते हुए संस्कार, छीजते हुए आपसी सम्बन्ध, दम तोड़ती हुई संवेदनाएँ, चरमराता हुआ सामाजिक ढाँचा, सुख-सुविधाओं की बदलती हुए परिभाषाएँ, शब्दों के बदलते हुए अर्थ, अपना महत्त्व खोती हुई संस्थापित मान्यताएँ...सभी कुछ तो बदलता जा रहा है।...बदलना भी चाहिए। बदलाव तो प्रकृति का नियम है। हर चीज़ हर क्षण बदल रही है। हमारे लिए महत्त्व सिर्फ़ इसी बात का है कि बदलाव बेहतरी के लिए है या बदतरी के लिए, वो हमें ऊँचा उठाएगा या नीचे की तरफ़ ले जाएगा। बदलाव अच्छा है या बुरा...अब अच्छे और बुरे को भी अपने-अपने ढंग से परिभाषित करने लगे हैं लोग। यह भी एक अंतहीन बहस का विषय है...पर अपनी बात का विषय तो यह है भी नहीं। मैं तो बात कर रहा था वृद्धाश्रमों की। देखा जाए तो इसे भी तेज़ी से पसरते हुए बदलाव का ही एक हिस्सा माना जा सकता है, जो शायद अगले कुछ वर्षों में एक अनिवार्यता बन कर रहा जाएगा, समाज के एक उपेक्षित अंग के रूप में। विशेषकर बड़े शहरों में। इस पर भी अच्छे-बुरे का ठप्पा लगाना मैं नहीं चाहूँगा। मैं हूँ भी कौन यह ठप्पा लगाने वाला। लेकिन उस अंग को जन्म देने वाली भावनाओं, विचारों और कारणों पर विचार करना समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है।’’
बड़ी देर से चुपचाप सुन रही आरती ने कहा था, ‘‘कारण तो मुख्य यही है कि रहने के लिए जगह की कमी, छोटे मकान।’’
‘‘नहीं बेटे, यह एक कारण ज़रूर है, लेकिन मुख्य नहीं। कारण तो अनेकानेक हैं। देश की बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी, सरकार की लचर और असफल नीतियाँ, नेताओं का सत्ता-मोह, समाज का अपने कर्तव्यों के प्रति विमुखता का भाव, जन-साधारण का विदेशी संस्कृति के प्रति अंधा आकर्षण, भौतिकवाद की चकाचौंध में अच्छे-बुरे की तमीज़ खो बैठना, छोटी जगहों में अवसरों का अभाव, बड़े शहरों की तरफ़ जनता का पलायन और फिर नतीजतन तंग होते हुए मकान, तंग होते हुए दिल, बढ़ता हुआ स्वार्थ, भ्रष्टाचार और अनैतिकता, आर्थिक कठिनाइयाँ, और इन्हीं सबके चलते उपयोगी और अनुपयोगी का तीखा आकलन, वस्तुओं को ही नहीं, व्यक्तियों को भी निजी फ़ायदे-नुक़सान के तराज़ू में तौलकर देखने की, निर्दयता की हद तक बढ़ती हुई प्रवृत्ति...इसी तरह के अनेक बड़े ही ठोस कारण हैं जिनकी जड़ें समाज में काफ़ी गहरी उतर चुकी हैं।’’
आरती बड़ी सोच में डूबी हुई सी लगी। कुछ पलों के मौन के बाद मैंने ही फिर कहा था, ‘‘यह कहते हुए भी मुझे कोई संकोच नहीं कि उपेक्षित बुज़ुर्गों में से अधिकतर ख़ुद भी अपने आप को परिवार के लिए किसी रूप में उपयोगी बनाए रखने के बारे में उदासीन ही रहते हैं। बदलते हुए परिवेश में अपने आप को ढालने की कोशिश उन्होंने ख़ुद भी कभी नहीं की होगी। इसलिए उनकी दुर्दशा के लिए उनके बाद की पीढ़ी को ही शतप्रतिशत दोषी मान लेना, शायद न्यायसंगत नहीं होगा।’’
हम वृद्धाश्रम पहुँच गए थे। परिसर में एक तरफ़ कार रोकते हुए आरती ने कहा, ‘‘मैं आती हूँ दसेक मिनिट में। आप बैठिए।’’
कहना चाहता था कि तुम अपने आप को किसी समय सीमा में मत बाँधो। आराम से अपना काम करके आओ। वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने ही काम इतने रहते हैं। फ़ालतू तो तुम बैठोगी भी नहीं।...लेकिन अपना ही सोचा हुआ ग़ैर-ज़रूरी-सा लगा, और सिर्फ़ ‘हूँ’ कहके रह गया था। आरती कार का एअर कंडीशनर चलता ही छोड़ गई थी, ताकि मुझे गर्मी न लगे। हवा का वेग सीधा मेरे चेहरे पर पड़ा रहा था। मैंने उसकी दिशा बदल दी। कार के अन्दर काफ़ी ठंड होते हुए भी मुझे कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। वैसे भी कृत्रिम हवा की बनिस्बत स्वाभाविक हवा मुझे ज़्यादा पसंद है। मैंने एअर कंडीशनर बंद कर दिया। पास की खिड़की का शीशा उतार दिया। बाहरी हवा के हल्के से झोंके ने काफ़ी राहत पहुँचाई। बाहर झाँका तो कुछ दूर पर बरामदे की सीढ़ियों के पास एक कुतिया सोई हुई थी। चार पिल्ले उसके स्तनों को चिचोड़ रहे थे। मुझे अचानक लेसी की याद आ गई। हमारी ही कॉलोनी के मिस्टर नायर जब वहाँ की छोटी-सी कॉटेज छोड़ कर बोरीवली के नए फ़्लैट में गए तो लेसी को आवारा घूमने के लिए छोड़ गए थे। किसी बढ़िया नस्ल की तो थी भी नहीं बेचारी, जिसके पिल्ले बेचकर कुछ कमा सकते। नए फ़्लैट में तीन पिल्लों के साथ यह आवारा कुतिया...ना रे बाबा ना...। सुना था कि मिस्टर नायर जब सारा सामान ट्रक पर लदवा कर घर से निकले तो लेसी बड़ी सड़क तक ट्रक के पीछे दौड़ती हुई गई थी। सड़क पर पहुँचकर वो रुकी, ट्रक को ओझल होता हुआ देखती रही। फिर लौट आई थी, निराश, उदास। शायद बच्चों का मोह उसके पैरों की बेड़ी बन गया होगा। उसी दिन से कॉलोनी में दर-दर जाकर उसने भीख माँगी। किसी ने टुकड़ा डाला, किसी ने दुत्कार दिया। जैसे-तैसे उसने बच्चों को पाला, लेकिन कॉलोनी छोड़कर कहीं गई नहीं।...फिर एक दिन नगरपालिका की कुत्ता-गाड़ी आई और पिल्लों को उठाकर ले गई।...लेसी किसी तरह उनकी निगाहों से बच गई थी।....
पता नहीं लेसी की कौन-सी नैसर्गिक प्रतिभा द्वारा उसे यह बोध हो गया कि कई सालों से महानगर में रहने के बावजूद मेरा पशुप्रेम अभी ज़िन्दा है। अगली सुबह परिसर का द्वार खुला देखकर वो घर के बरामदे तक आ पहुँची। मेरी नज़रों में नज़रें गड़ाए रही थोड़ी देर। उसकी पनीली उदास आँखों में गहरी वेदना के साथ-साथ हार्दिक प्रार्थना के स्वर भी ठहरे से लगे। मानो कह रही हो, बहुत आशाओं के साथ तुम्हारे द्वार पर आई हूँ। मिलेगा तुम्हारे घर में सहारा विपदा की मारी इस अबला को ? देखो, मैं बेवफ़ा नहीं हूँ, कामचोर भी नहीं। सहारा दोगे तो...
मैं ज़्यादा देर तक उसकी तरफ़ देख नहीं पाया। हाथ की किताब मेज़ पर छोड़कर मैं उठा। रसोईघर में से दो बासी रोटियाँ लाकर उसके सामने रख दीं। वो ख़ुशी से नाच उठी। तेज़ी से पूँछ हिला-हिलाकर वो मेरे पैरों में लोट-पोट होने लगी। मैं हैरान था, रोटियों पर झटपने की बजाय वो इन औपचारिकताओं में क्यों उलझ गई। मैंने कहा, ‘बस-बस, अब खाना खा लो। भूख लगी होगी।’ उसने फिर मेरी तरफ़ देखा। उसकी आँखों में ख़ुशी की चमक थी। उसकी पूँछ तब भी बदस्तूर हिल रही थी। मैं कुर्सी पर जा बैठा। मेरे दोबारा कहने पर ही उसने रोटी को मुँह लगाया। खा चुकी तो उसने मेरी तरफ़ एक बार देखा। मैंने कहा, ‘और खाना तो अब दोपहर को ही मिलेगा, जब ताज़ा बनेगा।’ मुझे लगा, वो मेरी बात समझ गई है। वो उठी। उसने फिर कई बार पूँछ हिलाकर मेरा आभार माना, और चुपचाप कॉटेज के परिसर की अढ़ाई फुट ऊँची दीवार चढ़कर दरवाज़े के पास जा बैठी।...उसके बाद दस साल तो ज़िन्दा रही होगी वो। उस अर्से में मुझे न तो किसी चौकीदार की ज़रूरत महसूस हुई और न दरवाज़े पर घंटी की। आने वाला कुछ दूर ही होता जब वो उसे सावधान कर देती और हम लोगों को किसी मेहमान के आने की संभावना से सूचित। आने वाला पहचान का होता तो पूँछ हिलाते-हिलाते, बड़े सम्मान के साथ उस बरामदे तक लेके आती, लेकिन आगंतुक अगर अनजाना हुआ तो उसे अन्दर दाख़िला दिलवाने के लिए किसी घरवाले को द्वार तक जाना होता था।....अपनी जगह वो कभी-कभार ही छोड़ती थी। या तो जब खाने के लिए उसे बरामदे में बुलाया जाता या फिर जब बारिश ज़्यादा हो रही होती तब वो बरामदे में आ बैठती। उस समय भी उसने अपने फ़र्ज़ में कोताही कभी नहीं बरती। निगाहें लगातार उसकी दरवाज़े पर ही रहतीं। वैसे में भी कोई आता तो उसके दरवाज़ा खोलने से पहले ही वो वहाँ तैनात हो जाती, सरहद पर खड़े सिपाही की तरह।
पता नहीं मेरी सोच का सिलसिला और कितनी देर लेसी के ही इर्द-गिर्द रहता, पर तभी एक आदमी एक बड़ा-सा थैला लिए सामने से गुज़रा। मूली के हरे पत्ते मटमैले रंग के थैले में से बाहर झाँक रहे थे। मैं जान गया कि वो सब्ज़ियाँ लेकर आया है। वो आदमी बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़कर मकान के पिछले हिस्से की तरफ़ चला गया। मैंने अनुमान लगाया कि रसोईघर उसी तरफ़ होगा। कुछ देर के बाद उसी ओर से कुछ बरतनों के उठाने-धरने और दो-तीन व्यक्तियों के बोलने की मिलीजुली अस्पष्ट-सी आवाज़ें सुनाई दीं और वो लेटी हुई कुतिया अचानक उठकर अपने बच्चों से पीछा छुड़ाती हुई उसी दिशा में लपक ली, तो रसोईघर का उधर होना निश्चित हो गया।
तभी ख़याल आया, कहीं भी हो रसोईघर या खाने का कमरा या सोने का, मुझे क्या लेना देना ? क्यों सोच रहा हूँ मैं ये फ़िज़ूल की बातें ?
कार की खिड़की से सिर ज़रा बाहर निकाला और ऊपर की तरफ़ देखना चाहा। आस-पास की ऊँची-ऊँची इमारतों ने निगाहें आकाश तक पहुँचने नहीं दीं। कुछ बंद, कुछ खुली, कुछ अधखुली खिड़कियों पर तैरती हुई नज़रें, धरातल पर उतरते-उतरते, आश्रम के अंतिम छोर की पहली मंज़िल के कमरे की खिड़की पर अटक के रह गईं। सरदल से सिर टिकाए एक नारी आकृति दिखाई दी। जिस ज़ाविये से वो मुझे दिखाई दे रही थी, शायद वही उसके चेहरे का सबसे ख़ूबसूरत कोण था। लम्बी-सी सुतवाँ नाक, पतले-पतले होंठ, कुछ घुँघराले बिखरे हुए से सफ़ेद बाल, गेहुआँ रंग जिसमें बाहर से आती हुई रोशनी ने कुछ दमक सी पैदा कर दी थी। कहीं दूर कुछ खोजती हुई सी उदास नज़रें। पृष्ठभूमि में कमरे का नीम अँधेरा...मैंने देखा तो उस आकृति को देखता ही रह गया। दरअसल स्तंभित सा हो गया था मैं।...हे भगवान ! तू भी अजीब खेल खेलता है। इतनी ख़ूबसूरत नारी, यहाँ वृद्धाश्रम में ? कुछ तो सोचा होता उसे यहाँ तक पहुँचाने से पहले। लगता है दिल या दया जैसी कोई चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं भगवान। पता नहीं न्याय की कौन-सी तराज़ू में तौलते हो तुम सब कुछ।
फिर ख़याल आया, खण्डहरों में भी फूल खिलते हैं, ख़ूबसूरत फूल, मनमोहक फूल...
तभी अचानक मुझे बहुत साल पहले देखी हुई अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग याद आ गई। इसी तरह चौखट से लगी खड़ी थी वो नारी। कुछ इसी तरह की मुद्रा, कुछ इसी तरह की भाव-भंगिमा। कुछ इसी तरह अतीत के गह्वरों में भटकती हुई निगाहें। बस, एक ही फ़र्क़ था, मोटे से तौर पर। वो नारी यौवन के द्वार पर थी और यह बुढ़ापे की कगार पर।...कल्पना-कल्पना में ही मैंने अमृता की उस पेंटिंग को लाकर खिड़की के पास खड़ा कर दिया। देखता रहा कुछ देर बड़े ध्यान से दोनों को। कभी इसे, कभी उसे। कभी दोनों को एक साथ। खिड़की की वृद्धा, पेंटिंग की यौवना से किसी तरह भी कम नहीं थी।
फिर अकस्मात मुझे दुःख और पश्चात्ताप ने घेर लिया। काश ! आज मैं अपना कैमरा साथ लाया होता। यहीं बैठे-बैठे, ज़ूम लैंस, लगाकर इतनी ख़ूबसूरत तस्वीर उतारी जा सकती थी कि...जो भी देखता, वाह-वाह कर उठता। उसका आदमक़द ऐनलार्जमेंट करवा के अपने घर में ढाँग लेता। अमृता की आत्मा भी कभी देखती तो अचंभे में आ जाती। बेसाख़्ता उसके मुँह से निकलता, हे वाहे गुरु ! मेरी वो पेंटिंग बुढ़िया कैसे गई ?
ख़ैर, बात पूरी सुना दूँ तो आप ख़ुद ही फ़ैसला कीजिएगा।
उस दिन सब से पहली बात तो यह हुई कि नाश्ता करने बैठा ही था जब टेलीफ़ोन की घंटी घनघनाई। चम्मच की जगह चोग़ा उठाया। बिटिया की आवाज़ थी, ‘‘शहर चलते हैं क्या ?’’
कुछ अचंभा सा हुआ था। कहा, ‘‘काम तो कोई है नहीं। क्या करूँगा जाकर ? व्यर्थ की थकावट....साढ़े तीन-चार घंटे का आना-जाना और...’’
‘‘ठीक है। मैंने तो यूँ ही पूछा। बहुत दिनों से कहीं आए-गए नहीं न आप। घर में बैठे-बैठे....’’
‘‘आज तो रहने ही दो।’’ एक तरह से उसी के शब्द मेरी ज़बान पर आ गए थे, अनचाहे।
उन लोगों का शहर आना-जाना तो लगा ही रहता है। रोज़ नहीं तो हफ़्ते में कम-से-कम तीन-चार दिन। कभी वो, कभी उसके पतिदेव, या कभी दोनों। मैंने उसे अकेली जाते देख एक बार पूछा, ‘‘चलूँ तुम्हारे साथ ?’’ तो उसका जवाब था, ‘‘नहीं-नहीं, बहुत थक जाएँगे आप। ट्रैफ़िक इतना बढ़ गया है कि जगह-जगह ट्रैफ़िक जाम। बैठे-बैठे उकताहट होने लगती है। कार का सफ़र भी अब आनंददायक नहीं, एक मजबूरी है। वैसे आप को कुछ काम है शहर में ? मुझे बताइए, मैं करती आऊँगी।’’
‘‘नहीं-नहीं, काम कोई नहीं। वो तो तुम अकेली...’’
‘‘ओह दादा...आप भी बस...अब मैं बड़ी हो गई हूँ, और वैसे भी मेरी फ़िक्र करने वाला अब यह है न।’’
उसने अपने पति की ओर इशारा किया था। दोनों मुस्कराए थे। बिटिया ने जोड़ा था, ‘‘आज भी मैं अकेली नहीं जा रही। ड्राइवर है मेरे साथ।’’
टेलीफ़ोन रख के मैं नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद एक अजीब सा अहसास हुआ। सारा घर जैसे घुटन से भर गया है। गर्मी और उमस बढ़ती जा रही है।...हवा एकदम बंद। मेरी निगाहें छत की तरफ़ उठीं। पंखा तो चल रहा था। मैंने उठकर रफ़्तार तेज़ कर दी। लेकिन घुटन और उमस में कोई फ़र्क नहीं हुआ।...कुछ अजीब सी बेचैनी, जो बढ़ती ही जा रही थी।
मैंने नाश्ता बीच में ही छोड़कर फ़ोन पर नम्बर घुमाया। कुछ देर बाद कहा था, ‘‘ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कितने बजे निकलेंगे ?’’
‘‘मुंबई का कार्यक्रम तो आज का रद्द हो गया, दादा। अब शायद सोम या मंगल को जाएँ।’’
‘‘अच्छा !’’
‘‘वैसे मैं सांताक्रूज़ तक जा रही हूँ। आप ड्राइव के तौर पर चलना चाहें तो...’’
‘‘किस समय ?’’
‘‘यही...कोई ग्यारह बजे।’’
‘‘ठीक है, मैं तैयार रहूँगा।’’
लगा जैसे ज़बरदस्ती ही उगलवाया हो वो वाक्य किसी ने मुझसे। भीतर-ही-भीतर एक द्वन्द्व सा चलता रहा था कुछ देर। अपने ही अन्दर से एक आवाज़ सुनाई दी थी, ‘अब सांताक्रूज़ में क्या काम है तुम्हें जो झट तैयार हो गए ?’
‘हो गया तैयार तो तुम्हें क्या ?’’
‘‘नहीं-नहीं, मुझे क्या। तुम्हीं कहा करते हो, बिना काम के कहीं जाने का क्या मतलब अब थकोगे नहीं ?’’
‘ओहो तुम भी...’’
‘‘तुम तो बुरा मान गए दोस्त। अपना समझता हूँ इसीलिए कहा। अब इतना क्यों सोच रहे हो ? चाहो तो अब भी फ़ोन उठाओ और मना कर दो।’
‘नहीं, नहीं, नहीं। नहीं करूँगा मना। मुझे जाना है तो बस जाना है। चुप रहो तुम।’
‘ह...ह...ह’
कुछ देर बाद मुझे लगा था, यह बच्चे की-सी ज़िद क्यूँ ? कौन-सी ऐसी मजबूरी है जो आज स्वभाव के विपरीत मुझे इस दुविधा में डाले हुए है ? इतनी साधारण-सी बात पर इतना डाँवाडोल तो कभी नहीं पाया था मैंने अपने आप को। मेरी तो हर बात सीधी-सपाट हुआ करती है हमेशा। दो टूक, इधर या उधर। लेकिन आ तमाम क्रियाएँ जैसे मैं नहीं कर रहा, कोई और करवा रहा है मुझसे।
रास्ते में मैंने आरती से पूछा, ‘‘मुंबई जाते-जाते सांताक्रूज़ का प्रोग्राम कैसे बन गया ?’’
‘‘मुबंई का कार्यक्रम तो सिर्फ़ मुल्तवी हुआ है। पहले सोचा था शाम को लौटते हुए थोड़ी देर सांताक्रूज़ रुक लूँगी। वो अपनी ज्योत्सना है न, टाइपिस्ट, कितने ही दिनों से कह रही थी, उसका कोई रिश्तेदार है। बेचारों के पास मकान तो हैं छोटा-सा, एक कमरे का, और रहने वाले हैं पाँच। गाँव से बूढ़ी माँ को भी लाना पड़ा, जिसे अब वे वृद्धाश्रम में रखना चाहते हैं। मेरी वहाँ पहचान है, इसलिए...।’’
वृद्धाश्रम की बात से ज़रूर मेरे चेहरे पर कुछ बदलाव आया होगा, जिसे महसूसते हुए आरती ने क्षमा-याचना के से स्वर में तुरन्त ही कहा, ‘‘मुझे बिलकुल याद नहीं रहा कि वृद्धाश्रम में जाना आपको अच्छा नहीं लगता। ख़ैर, जुहू का एक चक्कर लगा के लौट चलते हैं। आश्रम में मैं फिर कभी हो आऊँगी, कल-वल।’’
‘‘नहीं-नहीं, तुम जिस काम के लिए निकली हो उसे कर ही डालो। मैं कार में बैठा रहूँगा।’’
‘‘पक्का ?’’
‘‘बिल्कुल पक्का ।’’
‘‘पिछली बार की तरह न हो। हफ़्ता-भर तक आपकी उदासी नहीं टूटी थी। हर समय वही सोच, वही बात।...वही माहौल छाया रहा था दिलो-दिमाग़ पर आपके।’’
‘‘वो तो बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, आरती। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के साथ वही होता जो मेरे साथ हुआ। अब तुम भी कभी बालाश्रम में खाना और मिठाई लेकर जाती हो, कभी वृद्धों के लिए वस्त्र इकट्ठे करती हो, चीनी-चावल दे आती हो, यह भी तुम्हारी संवेदनशीलता का ही सक्रियात्मक रूप है।...और यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि वहाँ जाना मुझे अच्छा नहीं लगा था। हाँ, दुःख ज़रूर हुआ था उन्हें देखकर। एक उदास, उजाड़-सा माहौल। मुर्झाए हुए चेहरे, धँसी हुई आँखें, झुके हुए माथे, मजबूरी और लाचारी की मुजस्सम तस्वीरें। कुछ खोजती हुई, कुछ पूछती हुई-सी उनकी पनीली निगाहें। अपनों से कटे हुए दूर। अपने आप को तिलतिल करके मिटता हुआ देखने के लिए विवश, जैसे कण-कण करके चुकते हुए तेल और तिलतिल करके जलती हुई बाती का साक्षी मिट्टी का दिया। बुढ़ापा तो ज़िन्दगी की ही नौ अवस्थाओं में से एक है, फिर इतना उपेक्षित क्यूँ ? क्या इसीलिए कि उसकी उपयोगिता कम हो गई है, या बिलकुल नहीं रही ?...हमने तो संयुक्त परिवारों का दौर भी देखा है आरती, जहाँ बुढ़ापे की अहमियत और बढ़ जाती थी। परिवार की कोई भी समस्या हो, राय-मशविरे और हल के लिए निगाहें बुजुर्गों की तरफ़ ही उठती थीं। उन्हें अनुभव का ख़ज़ाना और उनके शब्दों को जीवन का निचोड़ समझा जाता था।...पर अब ज़माना बहुत बदल गया है। बल्कि बदलता ही चला जा रहा है, हर रोज़, बड़ी तेज़ी के साथ।...टूटते हुए परिवार, विखंडित होते हुए संस्कार, छीजते हुए आपसी सम्बन्ध, दम तोड़ती हुई संवेदनाएँ, चरमराता हुआ सामाजिक ढाँचा, सुख-सुविधाओं की बदलती हुए परिभाषाएँ, शब्दों के बदलते हुए अर्थ, अपना महत्त्व खोती हुई संस्थापित मान्यताएँ...सभी कुछ तो बदलता जा रहा है।...बदलना भी चाहिए। बदलाव तो प्रकृति का नियम है। हर चीज़ हर क्षण बदल रही है। हमारे लिए महत्त्व सिर्फ़ इसी बात का है कि बदलाव बेहतरी के लिए है या बदतरी के लिए, वो हमें ऊँचा उठाएगा या नीचे की तरफ़ ले जाएगा। बदलाव अच्छा है या बुरा...अब अच्छे और बुरे को भी अपने-अपने ढंग से परिभाषित करने लगे हैं लोग। यह भी एक अंतहीन बहस का विषय है...पर अपनी बात का विषय तो यह है भी नहीं। मैं तो बात कर रहा था वृद्धाश्रमों की। देखा जाए तो इसे भी तेज़ी से पसरते हुए बदलाव का ही एक हिस्सा माना जा सकता है, जो शायद अगले कुछ वर्षों में एक अनिवार्यता बन कर रहा जाएगा, समाज के एक उपेक्षित अंग के रूप में। विशेषकर बड़े शहरों में। इस पर भी अच्छे-बुरे का ठप्पा लगाना मैं नहीं चाहूँगा। मैं हूँ भी कौन यह ठप्पा लगाने वाला। लेकिन उस अंग को जन्म देने वाली भावनाओं, विचारों और कारणों पर विचार करना समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है।’’
बड़ी देर से चुपचाप सुन रही आरती ने कहा था, ‘‘कारण तो मुख्य यही है कि रहने के लिए जगह की कमी, छोटे मकान।’’
‘‘नहीं बेटे, यह एक कारण ज़रूर है, लेकिन मुख्य नहीं। कारण तो अनेकानेक हैं। देश की बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी, सरकार की लचर और असफल नीतियाँ, नेताओं का सत्ता-मोह, समाज का अपने कर्तव्यों के प्रति विमुखता का भाव, जन-साधारण का विदेशी संस्कृति के प्रति अंधा आकर्षण, भौतिकवाद की चकाचौंध में अच्छे-बुरे की तमीज़ खो बैठना, छोटी जगहों में अवसरों का अभाव, बड़े शहरों की तरफ़ जनता का पलायन और फिर नतीजतन तंग होते हुए मकान, तंग होते हुए दिल, बढ़ता हुआ स्वार्थ, भ्रष्टाचार और अनैतिकता, आर्थिक कठिनाइयाँ, और इन्हीं सबके चलते उपयोगी और अनुपयोगी का तीखा आकलन, वस्तुओं को ही नहीं, व्यक्तियों को भी निजी फ़ायदे-नुक़सान के तराज़ू में तौलकर देखने की, निर्दयता की हद तक बढ़ती हुई प्रवृत्ति...इसी तरह के अनेक बड़े ही ठोस कारण हैं जिनकी जड़ें समाज में काफ़ी गहरी उतर चुकी हैं।’’
आरती बड़ी सोच में डूबी हुई सी लगी। कुछ पलों के मौन के बाद मैंने ही फिर कहा था, ‘‘यह कहते हुए भी मुझे कोई संकोच नहीं कि उपेक्षित बुज़ुर्गों में से अधिकतर ख़ुद भी अपने आप को परिवार के लिए किसी रूप में उपयोगी बनाए रखने के बारे में उदासीन ही रहते हैं। बदलते हुए परिवेश में अपने आप को ढालने की कोशिश उन्होंने ख़ुद भी कभी नहीं की होगी। इसलिए उनकी दुर्दशा के लिए उनके बाद की पीढ़ी को ही शतप्रतिशत दोषी मान लेना, शायद न्यायसंगत नहीं होगा।’’
हम वृद्धाश्रम पहुँच गए थे। परिसर में एक तरफ़ कार रोकते हुए आरती ने कहा, ‘‘मैं आती हूँ दसेक मिनिट में। आप बैठिए।’’
कहना चाहता था कि तुम अपने आप को किसी समय सीमा में मत बाँधो। आराम से अपना काम करके आओ। वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने ही काम इतने रहते हैं। फ़ालतू तो तुम बैठोगी भी नहीं।...लेकिन अपना ही सोचा हुआ ग़ैर-ज़रूरी-सा लगा, और सिर्फ़ ‘हूँ’ कहके रह गया था। आरती कार का एअर कंडीशनर चलता ही छोड़ गई थी, ताकि मुझे गर्मी न लगे। हवा का वेग सीधा मेरे चेहरे पर पड़ा रहा था। मैंने उसकी दिशा बदल दी। कार के अन्दर काफ़ी ठंड होते हुए भी मुझे कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। वैसे भी कृत्रिम हवा की बनिस्बत स्वाभाविक हवा मुझे ज़्यादा पसंद है। मैंने एअर कंडीशनर बंद कर दिया। पास की खिड़की का शीशा उतार दिया। बाहरी हवा के हल्के से झोंके ने काफ़ी राहत पहुँचाई। बाहर झाँका तो कुछ दूर पर बरामदे की सीढ़ियों के पास एक कुतिया सोई हुई थी। चार पिल्ले उसके स्तनों को चिचोड़ रहे थे। मुझे अचानक लेसी की याद आ गई। हमारी ही कॉलोनी के मिस्टर नायर जब वहाँ की छोटी-सी कॉटेज छोड़ कर बोरीवली के नए फ़्लैट में गए तो लेसी को आवारा घूमने के लिए छोड़ गए थे। किसी बढ़िया नस्ल की तो थी भी नहीं बेचारी, जिसके पिल्ले बेचकर कुछ कमा सकते। नए फ़्लैट में तीन पिल्लों के साथ यह आवारा कुतिया...ना रे बाबा ना...। सुना था कि मिस्टर नायर जब सारा सामान ट्रक पर लदवा कर घर से निकले तो लेसी बड़ी सड़क तक ट्रक के पीछे दौड़ती हुई गई थी। सड़क पर पहुँचकर वो रुकी, ट्रक को ओझल होता हुआ देखती रही। फिर लौट आई थी, निराश, उदास। शायद बच्चों का मोह उसके पैरों की बेड़ी बन गया होगा। उसी दिन से कॉलोनी में दर-दर जाकर उसने भीख माँगी। किसी ने टुकड़ा डाला, किसी ने दुत्कार दिया। जैसे-तैसे उसने बच्चों को पाला, लेकिन कॉलोनी छोड़कर कहीं गई नहीं।...फिर एक दिन नगरपालिका की कुत्ता-गाड़ी आई और पिल्लों को उठाकर ले गई।...लेसी किसी तरह उनकी निगाहों से बच गई थी।....
पता नहीं लेसी की कौन-सी नैसर्गिक प्रतिभा द्वारा उसे यह बोध हो गया कि कई सालों से महानगर में रहने के बावजूद मेरा पशुप्रेम अभी ज़िन्दा है। अगली सुबह परिसर का द्वार खुला देखकर वो घर के बरामदे तक आ पहुँची। मेरी नज़रों में नज़रें गड़ाए रही थोड़ी देर। उसकी पनीली उदास आँखों में गहरी वेदना के साथ-साथ हार्दिक प्रार्थना के स्वर भी ठहरे से लगे। मानो कह रही हो, बहुत आशाओं के साथ तुम्हारे द्वार पर आई हूँ। मिलेगा तुम्हारे घर में सहारा विपदा की मारी इस अबला को ? देखो, मैं बेवफ़ा नहीं हूँ, कामचोर भी नहीं। सहारा दोगे तो...
मैं ज़्यादा देर तक उसकी तरफ़ देख नहीं पाया। हाथ की किताब मेज़ पर छोड़कर मैं उठा। रसोईघर में से दो बासी रोटियाँ लाकर उसके सामने रख दीं। वो ख़ुशी से नाच उठी। तेज़ी से पूँछ हिला-हिलाकर वो मेरे पैरों में लोट-पोट होने लगी। मैं हैरान था, रोटियों पर झटपने की बजाय वो इन औपचारिकताओं में क्यों उलझ गई। मैंने कहा, ‘बस-बस, अब खाना खा लो। भूख लगी होगी।’ उसने फिर मेरी तरफ़ देखा। उसकी आँखों में ख़ुशी की चमक थी। उसकी पूँछ तब भी बदस्तूर हिल रही थी। मैं कुर्सी पर जा बैठा। मेरे दोबारा कहने पर ही उसने रोटी को मुँह लगाया। खा चुकी तो उसने मेरी तरफ़ एक बार देखा। मैंने कहा, ‘और खाना तो अब दोपहर को ही मिलेगा, जब ताज़ा बनेगा।’ मुझे लगा, वो मेरी बात समझ गई है। वो उठी। उसने फिर कई बार पूँछ हिलाकर मेरा आभार माना, और चुपचाप कॉटेज के परिसर की अढ़ाई फुट ऊँची दीवार चढ़कर दरवाज़े के पास जा बैठी।...उसके बाद दस साल तो ज़िन्दा रही होगी वो। उस अर्से में मुझे न तो किसी चौकीदार की ज़रूरत महसूस हुई और न दरवाज़े पर घंटी की। आने वाला कुछ दूर ही होता जब वो उसे सावधान कर देती और हम लोगों को किसी मेहमान के आने की संभावना से सूचित। आने वाला पहचान का होता तो पूँछ हिलाते-हिलाते, बड़े सम्मान के साथ उस बरामदे तक लेके आती, लेकिन आगंतुक अगर अनजाना हुआ तो उसे अन्दर दाख़िला दिलवाने के लिए किसी घरवाले को द्वार तक जाना होता था।....अपनी जगह वो कभी-कभार ही छोड़ती थी। या तो जब खाने के लिए उसे बरामदे में बुलाया जाता या फिर जब बारिश ज़्यादा हो रही होती तब वो बरामदे में आ बैठती। उस समय भी उसने अपने फ़र्ज़ में कोताही कभी नहीं बरती। निगाहें लगातार उसकी दरवाज़े पर ही रहतीं। वैसे में भी कोई आता तो उसके दरवाज़ा खोलने से पहले ही वो वहाँ तैनात हो जाती, सरहद पर खड़े सिपाही की तरह।
पता नहीं मेरी सोच का सिलसिला और कितनी देर लेसी के ही इर्द-गिर्द रहता, पर तभी एक आदमी एक बड़ा-सा थैला लिए सामने से गुज़रा। मूली के हरे पत्ते मटमैले रंग के थैले में से बाहर झाँक रहे थे। मैं जान गया कि वो सब्ज़ियाँ लेकर आया है। वो आदमी बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़कर मकान के पिछले हिस्से की तरफ़ चला गया। मैंने अनुमान लगाया कि रसोईघर उसी तरफ़ होगा। कुछ देर के बाद उसी ओर से कुछ बरतनों के उठाने-धरने और दो-तीन व्यक्तियों के बोलने की मिलीजुली अस्पष्ट-सी आवाज़ें सुनाई दीं और वो लेटी हुई कुतिया अचानक उठकर अपने बच्चों से पीछा छुड़ाती हुई उसी दिशा में लपक ली, तो रसोईघर का उधर होना निश्चित हो गया।
तभी ख़याल आया, कहीं भी हो रसोईघर या खाने का कमरा या सोने का, मुझे क्या लेना देना ? क्यों सोच रहा हूँ मैं ये फ़िज़ूल की बातें ?
कार की खिड़की से सिर ज़रा बाहर निकाला और ऊपर की तरफ़ देखना चाहा। आस-पास की ऊँची-ऊँची इमारतों ने निगाहें आकाश तक पहुँचने नहीं दीं। कुछ बंद, कुछ खुली, कुछ अधखुली खिड़कियों पर तैरती हुई नज़रें, धरातल पर उतरते-उतरते, आश्रम के अंतिम छोर की पहली मंज़िल के कमरे की खिड़की पर अटक के रह गईं। सरदल से सिर टिकाए एक नारी आकृति दिखाई दी। जिस ज़ाविये से वो मुझे दिखाई दे रही थी, शायद वही उसके चेहरे का सबसे ख़ूबसूरत कोण था। लम्बी-सी सुतवाँ नाक, पतले-पतले होंठ, कुछ घुँघराले बिखरे हुए से सफ़ेद बाल, गेहुआँ रंग जिसमें बाहर से आती हुई रोशनी ने कुछ दमक सी पैदा कर दी थी। कहीं दूर कुछ खोजती हुई सी उदास नज़रें। पृष्ठभूमि में कमरे का नीम अँधेरा...मैंने देखा तो उस आकृति को देखता ही रह गया। दरअसल स्तंभित सा हो गया था मैं।...हे भगवान ! तू भी अजीब खेल खेलता है। इतनी ख़ूबसूरत नारी, यहाँ वृद्धाश्रम में ? कुछ तो सोचा होता उसे यहाँ तक पहुँचाने से पहले। लगता है दिल या दया जैसी कोई चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं भगवान। पता नहीं न्याय की कौन-सी तराज़ू में तौलते हो तुम सब कुछ।
फिर ख़याल आया, खण्डहरों में भी फूल खिलते हैं, ख़ूबसूरत फूल, मनमोहक फूल...
तभी अचानक मुझे बहुत साल पहले देखी हुई अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग याद आ गई। इसी तरह चौखट से लगी खड़ी थी वो नारी। कुछ इसी तरह की मुद्रा, कुछ इसी तरह की भाव-भंगिमा। कुछ इसी तरह अतीत के गह्वरों में भटकती हुई निगाहें। बस, एक ही फ़र्क़ था, मोटे से तौर पर। वो नारी यौवन के द्वार पर थी और यह बुढ़ापे की कगार पर।...कल्पना-कल्पना में ही मैंने अमृता की उस पेंटिंग को लाकर खिड़की के पास खड़ा कर दिया। देखता रहा कुछ देर बड़े ध्यान से दोनों को। कभी इसे, कभी उसे। कभी दोनों को एक साथ। खिड़की की वृद्धा, पेंटिंग की यौवना से किसी तरह भी कम नहीं थी।
फिर अकस्मात मुझे दुःख और पश्चात्ताप ने घेर लिया। काश ! आज मैं अपना कैमरा साथ लाया होता। यहीं बैठे-बैठे, ज़ूम लैंस, लगाकर इतनी ख़ूबसूरत तस्वीर उतारी जा सकती थी कि...जो भी देखता, वाह-वाह कर उठता। उसका आदमक़द ऐनलार्जमेंट करवा के अपने घर में ढाँग लेता। अमृता की आत्मा भी कभी देखती तो अचंभे में आ जाती। बेसाख़्ता उसके मुँह से निकलता, हे वाहे गुरु ! मेरी वो पेंटिंग बुढ़िया कैसे गई ?
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book