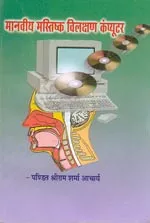|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटरश्रीराम शर्मा आचार्य
|
17 पाठक हैं |
||||||
शरीर से भी विलक्षण मस्तिष्क...
इसी प्रकार इन कोषों से दैनिक जीवन की आवश्यकताएँ पूरा कर सकने के लिए आवश्यक थोड़ा सा काम कर लिया जाता है, तो उतना ही करने में वे दक्ष रहते हैं। यदि अवसर मिला होता, उन्हें उभारा और प्रशिक्षित किया गया होता तो वे अबकी अपेक्षा लाखों गुनी क्षमता प्रदर्शित कर सके होते। अलादीन के चिराग की कहानी कल्पित हो सकती है, पर अपना मस्तिष्क सचमुच जादुई चिराग सिद्ध होता है।
मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर
शरीर से भी विलक्षण मस्तिष्क
यों तो मनुष्य शरीर अपने आप में ही परमात्मा की अद्भुत और विलक्षण कृति है।
मनुष्य शरीर जैसी समर्थ, सूक्ष्म बारीकियों से बनी हुई और स्वयं संचालित मशीन
बना पाना तो दूर रहा, इसकी संरचना को भी अभी समझ पाना संभव नहीं हो सका है।
इस विलक्षण और अद्भुत यंत्र का संचालन केंद्र है-'मस्तिष्क'। इस मस्तिष्क की
रचना मनुष्य शरीर से भी जटिल और विलक्षण है।
खोपड़ी की हड्डी से बनी टोकरी में परमात्मा ने इतनी महत्त्वपूर्ण सामग्री
सँजोकर रखी है कि उसे जादू की पिटारी कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी। शरीर
के अन्य किसी भी अवयव की अपेक्षा उसमें सक्रियता, चेतना और संवदेनशीलता की
इतनी अधिक मात्रा है कि उसे मानवीय सत्ता का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है।
रेलगाड़ी में जो महत्त्व इंजन का है वही अपने शरीर में मस्तिष्क का है।
डिब्बों की टूट-फूट हो जाने पर उन्हें सुधारने की या काटकर अलग कर देने की
व्यवस्था आसानी से हो जाती है, किंतु यदि इंजन खराब हो जाए तो सुयोग्य
इंजीनियर की देख-रेख में साधन-संपन्न कारखाने में ही उसकी मरम्मत हो सकती है।
जब तक मरम्मत न हो जाए तब तक रेलगाड़ी जहाँ की तहाँ खड़ी रहेगी, उसका थोड़ी
दूर आगे बढ़ सकना भी संभव न होगा।
शरीर में मस्तिष्क का वही स्थान है जो किसी बड़े कारखानों की मशीनों को बिजली
सप्लाई करने वाली शक्तिशाली मोटर का। मोटर बंद हो जाए या बिगड़ जाए, तो फिर
बिजली के अभाव में सारा कारखाना ही ठप्प हो जायेगा। शरीर के अन्य कलपुर्जों
में जो गतिशीलता दिखाई पड़ती है वह उनकी अपनी नहीं है। मस्तिष्क उन पर पूरी
तरह नियंत्रण रखता है। संचालन की प्रेरणा ही नहीं, शक्ति भी वहीं से मिलती
है।
मस्तिष्क को दो भागों में विभक्त माना जा सकता है। एक वह जिसमें मन और बुद्धि
काम करती है। सोचने-विचारने, तर्क-विश्लेषण और निर्णय करने की क्षमता इसी में
है। दूसरा भाग वह है, जिसमें आदतें संग्रहीत हैं और शरीर के क्रियाकलापों का
निर्देश निर्धारण किया जाता है। हमारी नाड़ियों में रक्त बहता है, हृदय
धड़कता है, फेफड़े श्वास-प्रश्वास क्रिया में संलग्न रहते हैं, मांसपेशियाँ
सिकुड़ती-फैलती हैं, पलक झपकते-खुलते हैं, सोने-जागने का, खाने-पीने और
मल-मूत्र त्याग का क्रम अपने ढर्रे पर अपने आप स्वसंचालित ढंग से चलता रहता
है। पर यह सब अनायास ही नहीं होता, इसके पीछे वह निरंतर सक्रिय मन नाम की
शक्ति काम करती है जिसे अचेतन मस्तिष्क कहते हैं। इसे ढर्रे का मन कह सकते
हैं। शरीर के यंत्र अवयव अपना-अपना काम करते रहने योग्य कलपुर्जी से बने हैं,
पर उनमें अपने आप संचालित रहने की क्षमता नहीं है, यह शक्ति मस्तिष्क के इसी
अचेतन मन से मिलती है। विचारशील मस्तिष्क तो रात में सो जाता है, विश्राम ले
लेता है। नशा पीने या बेहोशी की दवा लेने से मूर्छा ग्रसित हो जाता है।
उन्माद, आवेश आदि रोगों से ग्रसित भी वही होता रहता है। डॉक्टर इसी को
निद्रित करके आपरेशन करते हैं। किसी अंग विशेष में सुन्न करने की सुई लगाकर
भी इस बुद्धिमान् मस्तिष्क तक सूचना पहुँचाने वाले ज्ञान तंतु संज्ञा शून्य
कर दिये जाते हैं, फलतः पीड़ा का अनुभव नहीं होता और आपरेशन हो जाता है।
पागलखानों में इस चेतन मस्तिष्क का ही इलाज होता है। अचेतन की एक छोटी परत ही
मानसिक अस्पतालों की पकड में आई है वे इसे प्रभावित करने में भी थोड़ा-बहुत
सफल होते जा रहे हैं, किंतु उसका अधिकांश भाग प्रत्येक नियंत्रण से बाहर है।
पागल लोगों के शरीर की भूख, मल-त्याग, श्वास-प्रश्वास, रक्त-संचार तथा पलक
झपकना आदि क्रियाएँ अपने ढंग से होती रहती हैं। मस्तिष्क की विकृति का शरीर
के सामान्य क्रम संचालन पर बहुत कम असर पड़ता है।
मस्तिष्क अपने आप तो बहुत कुछ करता है, पर उसका विचारपूर्वक नियंत्रण एवं
उपयोग करना बहुत कम लोगों को बहुत थोड़ी मात्रा में आता है। वैज्ञानिकों का
कथन है कि मस्तिष्कीय चेतना पर ८ प्रतिशत नियंत्रण प्राप्त कर सकना प्रगतिशील
मनुष्य के लिए अभी तक संभव हो पाया है। उसकी ६२ प्रतिशत शक्ति ऐसी है जिस पर
नियंत्रण करना तो दूर उसकी ठीक तरह जानकारी भी प्राप्त नहीं की जा सकी है।
मनुष्य की बुद्धिमत्ता, साहसिकता, सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की जाती है।
अनुशासित मनोभूमि किस प्रकार प्रखर प्रतिभासंपन्न व्यक्तित्व के रूप में
विकसित होती है, यह भी सर्वविदित है। इतने पर भी इतना ही कहा माना जाता है कि
यह उसकी खोपड़ी में रखी हुई जादुई पिटारी का एक नगण्य सा चमत्कार है। यदि उसे
पूरी तरह जाना समझा जा सके, तो अबकी अपेक्षा वह हजारों गुनी अधिक विभूतियों
से भरा-पूरा हो सकता है।
लेकिन प्रगति का आधार इसी मस्तिष्कीय स्थिति पर निर्भर है। मूर्ख, मंदबुद्धि
और अनपढ़, अविकसित व्यक्ति या तो सुख के साधन कमा ही नहीं पाते और यदि किसी
प्रकार मिल भी जाये तो उनका समुचित सदुपयोग करके सुखी रह सकने की व्यवस्था
बना नहीं पाते, वे वस्तुएँ या परिस्थितियाँ उनके लिए जाल-जंजाल बन जाती हैं।
उपयोग की सही विधि न मालूम होने पर प्रयोग गलत होते हैं और गलती का परिणाम
विकृति एवं क्षति ही हो सकती है। संपदाएँ भी अविकसित मनःस्थिति होने पर किसी
को कोई सुख नहीं पहुंचा सकतीं। बारूद का खेल करने वाले जिस प्रकार
क्षतिग्रस्त होते हैं उसी प्रकार सांसारिक वैभव पाने पर भी मंद बुद्धि लोग
लाभान्वित नहीं होते, यों आमतौर से अच्छे सुविधा साधन मिलना ही उनके लिए कठिन
पड़ता है। इसके विपरीत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी
अभीष्ट साधन उपलब्ध कर लेते हैं। संपदाएँ पाते हैं, सुख भोगते हैं और
गौरवान्वित होते हैं। यह सब मस्तिष्कीय प्रखरता का ही वरदान है।
जिस मस्तिष्क पर हमारा वर्तमान और भविष्य पूरी तरह निर्भर है उसके संबंध में
लोग बहुत ही कम जानते हैं, बहुत ही कम ध्यान देते हैं। यह कितने आश्चर्य और
दुःख की बात है कि शरीर को परिपुष्ट बनाने के लिए कीमती भोजन जुटाया जाता है,
सुंदर बनने के लिए वस्त्राभूषण एवं श्रृंगार साधनों पर समय तथा धन लगाया जाता
है। इंद्रिय तृप्ति के लिए खर्चीले और समयसाध्य साधन जुटाये जाते हैं,
अन्यान्य सफलताओं के लिए घनघोर प्रयत्न किये जाते हैं, पर न जाने क्यों यह
अनुभव नहीं किया जाता कि मानसिक प्रखरता के बिना सारे काम औंधे सीधे होंगे और
उनके कठिन प्रयत्नों के फलस्वरूप जो सामग्री मिलेगी वह आनंददायक न होकर
विपत्ति का कारण बनेगी।
मानवीय मस्तिष्क में जितनी किस्म का, जितनी मात्रा में ज्ञान भरा रहता है
उसकी तुलना में संसार के बड़े से बड़े पुस्तकालय को भी तुच्छ ठहराया जा सकता
है। उलझे हुए प्रश्नों का न्यूनतम समय में उपयुक्त हल निकालने में संसार के
किसी सशक्त कंप्यूटर की तुलना उससे नहीं हो सकती। जरा से डिब्बे में भरी हुई
यह गुलाबी रंग की कढ़ी इतनी विलक्षण है कि उसकी समानता किसी भी बहुमूल्य
रासायनिक पदार्थ से नहीं की जा सकती।
मस्तिष्कीय क्रियाकलाप जिन नर्व सेल्स (तंत्रिका कोशिकाओं) से मिलकर संचालित
रहता है, उनकी संख्या प्रायः दस अरब होती है। इन्हें आपस में जोड़ने वाले
नर्व फाईवर (तंत्रिका तंत) और उनके इन्सुलेशन खोपड़ी के भीतर खचाखच भरे हुए
हैं। एक तंत्रिका कोशिका का व्यास एक इंच के हजारवें भाग से भी कम है और उसका
वजन एक औंस के साठ अरबवें भाग से अधिक नहीं है। तंत्रिका तंतुओं से होकर
बिजली के जो इंपल्स दौड़ते हैं, वही ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आवश्यक
सूचनाएँ उस केंद्र तक पहुंचाते हैं।
इन दस अरब कोशों को अद्भुत विशेषताओं से संपन्न देवदानव कहा जा सकता है।
इनमें से कुछ में तो माइक्रोफिल्मों की तरह न जाने कब-कब की स्मृतियाँ
सुरक्षित रहती हैं। मोटे तौर पर जिन बातों को हम भूल चुके होते हैं वे भी
वस्तुतः विस्मृत नहीं होतीं, वरन् एक कोने में छिपी पड़ी रहती हैं और जब अवसर
पाती हैं वर्षा की घास की तरह उभर कर ऊपर आ जाती हैं। केनेडा के स्नायु
विशेषज्ञ डॉ० पेनफील्ड ने एक व्यक्ति का एक स्मृति कोश विद्युत् धारा के
स्पर्श से उत्तेजित किया। उसने बीस वर्ष पहले देखी हई फिल्मों के कथानक और
गाने ऐसे सुनाये मानो अभी-अभी देखकर आया हो।
इन कोशों से संबंधित नाड़ी तंतु समस्त शरीर में फैले पड़े हैं। इन्हें दो
भागों में बाँटा जा सकता है 1-सेंसरी नर्वज-संज्ञा वाहक। 2-मोटर नर्वज-गति
वाहक। संज्ञा वाहक तंतुओं का संबंध ज्ञानेंद्रियों से होता है। जो कुछ हम
देखते, सुनते, चखते, सूंघते और स्पर्शानुभव करते हैं वह इन संज्ञा वाहकों के
माध्यम से संपन्न होता है और चलना, फिरना, खाना, नहाना, पढ़ना, लिखना आदि गति
वाहकों द्वारा। वे कर्मेंद्रियों को नियंत्रित एवं संचालित करते हैं।
यह मस्तिष्क सामान्य इंद्रियगम्य ज्ञान की जानकारियों तक सीमित है, ऐसा शरीर
विज्ञानियों द्वारा कहा जाता रहा है, पर अब न्यूरोलॉजी-पैरा
साइकोलाजी-मैटाफिजिक्स विज्ञान के जानकार यह स्वीकार करने लगे हैं कि मानवी
मन-विराट् विश्व मन का ही एक अंश है और जो कुछ उस विराट् ब्रह्मांड में हो
रहा है या निकट भविष्य में होने जा रहा है उसकी संवेदनाएँ मानवी मन को भी मिल
सकती हैं।
पिछले दिनों क्या-क्या हो चुका ? इस समय कहाँ क्या हो रहा है, और निकट भविष्य
में क्या होने की संभावनाएँ बन गईं ? उसे जान लेना किसी परिष्कृत मस्तिष्क के
लिए संभव है। हाँ-सामान्यतया यह अतींद्रिय अनुभूति प्रसुप्त स्थिति में पड़ी
रहती है। केवल वर्तमान से संबंधित प्रत्यक्ष का ही अधिक ज्ञान रहता है,
भूतकाल की निज से संबंधित घटनाएँ जब विस्मृत हो जाती हैं, तब अन्यत्र होने
वाली घटनाओं की जानकारी तो रहे ही कैसे ? पर यह बात केवल सामान्य स्तर के
मस्तिष्कों पर लागू होती है। परिष्कृत मस्तिष्क इससे कहीं ऊँचे उठे हुए होते
हैं और वे त्रिकालज्ञ की भूमिका प्रस्तुत कर सकते हैं।
उपलब्ध सूचनाएँ दफ्तर में रिकार्ड बनकर जमा नहीं होती रहतीं, वरन उन पर
तत्काल निर्णय करना होता है। इसके लिए सूचना कितने ही दफ्तरों, कितने ही
अफसरों के सामने से गुजरती हुई, उनको परामर्श, निर्देश नोट कराती हुई संबद्ध
अवयवों को सूचना देती है कि उन्हें इस संदर्भ में क्या करना है। आदेश ही
नहीं, आवश्यक साधन जुटाने की व्यवस्था भी इसी केंद्रीय निर्देशालय से होती
है। इंद्रियों द्वारा उपलब्ध सूचनाएँ और विचारों की हलचलें हर क्षण मस्तिष्क
को इतना अधिक कार्य व्यस्त रखती हैं कि इस सक्रियता पर आश्चर्यचकित रह जाना
पड़ता है। सिर पर इलेक्ट्रोड लगाकर भीतर चल रही हलचलों के जो चित्र
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम तैयार किये जाते हैं, उन्हें विद्युतीय तूफान की तरह
देखा जा सकता है।
बच्चों को मस्तिष्क की जानकारी टेलीफोन एक्सचेंज का उदाहरण देकर कराई जाती
है। बड़ों को उसे समझाना हो तो यों कहना चाहिए कि यदि अपने टेलीफोन का संबंध
संसार के समस्त टेलीफोनों से हो, अपनी बात समस्त टेलीफोनों से सुनी जाए और
उनके उत्तर एक साथ प्राप्त हों, सुने-समझे जायें तो उस स्थिति की तुलना
मस्तिष्कीय क्रियाकलाप से की जा सकती है।
मानव निर्मित सर्वोत्तम कंप्यूटर में अधिक से अधिक दस लाख इकाइयाँ होती हैं
और प्रत्येक इकाई के पाँच-छह से अधिक संपर्क सूत्र नहीं होते किंतु मस्तिष्क
में दस अरब कोशिकाएँ हैं। उनमें से प्रत्येक के लाखों-लाख संपर्क सूत्र हैं।
साथ ही प्रत्येक में जैव रसायनों के सम्मिश्रण में भारी भिन्नता भी है। घटित
होने वाली घटनाएँ और इंद्रिय संस्थानों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का निपटारा एक
अलग और सामयिक कार्य है। इसके अतिरिक्त श्वासोच्छ्वास, निद्रा, जागरण, हृदय
की धड़कन, रक्त संचार, पेशियों का आकुंचन- प्रकुंचन, शरीर कोशिकाओं का
जीवन-मरण आदि शरीर संचालन के इतने अधिक कार्य हैं जिन्हें बारीकी से देखने पर
समस्त संसार की सरकारों की संयुक्त व्यवस्था से भी अधिक सुविस्तृत ठहराया
जायेगा।
शरीर गत आवश्यकताओं और इनकी पूर्ति की क्रियाव्यवस्था मस्तिष्क का जो छोटा-सा
भाग सँभालता है, उसे "हाइपोथैलमस" कहते हैं। भूख, प्यास, नींद, मल विसर्जन,
पाचन आदि अनेकों क्रिया-कलाप इसी केंद्र से संचालित एवं व्यवस्थित किये जाते
हैं। मस्तिष्क के पिछले भाग में गुंबदाकार अंग "सेरिबेलम" इन हलचलों को
परस्पर संबद्ध करने वाले असंख्य सूत्रों को श्रृंखलाबद्ध करता है।
'चिंतन' का ज्ञान, स्मृति, बुद्धि, विवेचन, इच्छा आदि का कार्य-भार सँभालने
वाला अत्यंत विकसित भाग "सेरिबल फॉरर्टेक्स" कहलाता है। मस्तिष्कीय द्रव्य से
बनी हुई यह झुर्राकार परत मस्तिष्क के अग्रभाग और पार्यों में लिपटी हुई है।
इसकी मोटाई प्रायः एक मिली मीटर है। सूचनाओं का ग्रहण और निर्देशों का
प्रसारण करने में इस पट्टी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
तंत्रिका कोशाणु एक सफेद धागेयुक्त तंतु होता है। यह तंतु अन्यान्य न्यूरोनों
से जुड़ा होता है। इस प्रकार पूरा मस्तिष्क इन परस्पर जुड़े हुए धागों का एक
तंतु जाल बना हुआ है। इन्हीं सूत्रों से वे परस्पर संबद्ध रहते हैं और अपने
कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह परस्पर मिल-जुलकर करते हैं।
प्रत्येक प्रौढ़ मस्तिष्क प्रायः २० वाट विद्युत् शक्ति से चलता है। कुछ
कोषाणु विशेष रूप से इस बिजली को उत्पन्न करने का काम करते हैं और शेष उसका
उपयोग करके अपना काम चलाते हैं, वह एक सक्ष्म डायनामा है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन
का रासायनिक ईंधन जलाकर उसकी ऊर्जा को वे बिजली में परिवर्तित करते हैं।
कामचलाऊ मात्रा में वह कोषाणुओं को शक्ति प्रदान करती है और यदि उसकी
अनावश्यक मात्रा बन गई है तो स्वयं ही विसर्जित हो जाती है। उसका
चार्ज-डिस्चार्ज शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है।
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ की सहायता से यह जाना जा सकता है कि इस बिजली का
उत्पादन और उपभोग कहाँ, किस मात्रा में हो रहा है। इसमें घट-बढ़ हो जाने से
मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है अथवा यों भी कहा जा सकता है कि मानसिक संतुलन
बिगड़ने से इन विद्युत् धाराओं में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है।
सन् १9६८ में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क सम्मेलन आयोजित किया
गया था और संसार के विचारशील लोगों का ध्यान मस्तिष्कीय सुरक्षा एवं प्रगति
की ओर आकर्षित किया था। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉरन्यूरो-कैमिस्ट्री, ब्रेन एण्ड
बिहेवियर सोसाइटी, ब्रेन रिसर्च एसोसियेशन जैसी संस्थाओं ने उस वर्ष
मस्तिष्कीय गरिमा, संभावना, सुरक्षा एवं प्रगति के संबंध में अधिक
उत्साहपूर्वक काम किया था और जो कार्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में अब तक इस दिशा
में हो चुका है, उसका परिचय जनता को कराया था। इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ न्यूरो
बायोलॉजी, ब्रेन रिसर्च जनरल ऑफ न्यूरोबायोलॉजी जैसी विज्ञान पत्रिकाओं ने भी
अति महत्त्वपूर्ण लेख उस वर्ष प्रकाशित करके वैज्ञानिकों, सरकारों एवं
विचारशील लोगों को यह सुझाव दिया था कि मस्तिष्कीय गरिमा को अधिक
गंभीरतापूर्वक अनुभव किया जाए और उसे परिष्कृत करने की दिशा में अधिक काम
किया जाए।
मानवीय मस्तिष्क तीन पौंड से भी कम वजन का अखरोट जैसी आकृति का-दो गोलार्धों
में बँटा हुआ अनेक घुमावों वाला मांस पिंड है। एक को सेरिब्रेम दूसरे को
सेरिबेलम कहते हैं। तांत्रिकी कोशिकाओं से बना धूसर द्रव्य वाला यह पदार्थ
सूक्ष्म दर्शक यंत्र से देखने पर चित्र-विचित्र कोशिकाओं का रेगिस्तान जैसा
लगता है, इसके सारे कल-पुर्जे इस प्रकार तुड़े-मुड़े रखे हैं मानो वे आगे
बढ़ना चाहते हों, पर खोपड़ी की हड्डी ने उन्हें रोक दिया हो और वे
मुड़-तुड़कर गर्भस्थ बालक की तरह किसी प्रकार गुजारा कर रहे हों।
तीन महीने के भ्रूण का दिमाग मात्र पाँच ग्राम का होता है। छह महीने का होने
तक वह सौ ग्राम हो जाता है। जन्मते समय ३५० ग्राम का होता है। यह प्रौढ़
मनुष्य के मस्तिष्क का एक चौथाई है। अंततः मस्तिष्क चौदह सौ ग्राम तक जा
पहुंचता है। इससे प्रगट है कि आरंभिक जीवन में मस्तिष्कीय विकास कितनी तेजी
से होता है और पीछे वह कितना धीमा पड़ जाता है ? छह साल के बच्चे का दिमाग
प्रौढ़ता की स्थिति का पंचानबे प्रतिशत होता है। बीस वर्ष की आयु तक विकास
पूर्ण हो जाता है। पीछे तो वह परिपक्व और परिष्कृत भर होता रहता है।
पुरुष की तुलना में स्त्रियों का मस्तिष्क १०० ग्राम हल्का होता है। पर उसमें
शारीरिक वजन का अनुपात भर मानना चाहिए। स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा वजन में
हल्की होती हैं तदनुरूप मस्तिष्क भी हल्का होता है। वजन के आधार पर किसी को
विकसित अथवा अविकसित नहीं ठहराया जा सकता। संसार के प्राणियों में सबसे भारी
मस्तिष्क ह्वेल मछली का ७०00 ग्राम का होता है, इसके बाद ५००० ग्राम हाथी का
होता है। क्या उन्हें १४०० ग्राम वाले मनुष्य से अधिक बुद्धिमान् कहें ?
संसार भर में सबसे अधिक हल्की अपने नाटे कद के कारण जापानी महिलाएँ होती हैं,
उनका वजन औसतन ५० ग्राम कम अर्थात् १२५० ग्राम होता है, फिर भी वे संसार में
कहीं की भी नारियों से कम बुद्धिमान् नहीं होती हैं। वे अपने समाज में
पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं होती।
कुछ समय पूर्व बंबई के एक विद्वान् वी० जे० रेले ने एक पुस्तक लिखी थी-"दी
वैदिक गॉड्स एज फिगर्स ऑफ बायोलॉजी"-उसमें उसने सिद्ध किया था कि वेदों में
वर्णित आदित्य, वरुण, अग्नि, मरुत्, मित्र, अश्विनी, रुद्र आदि मस्तिष्क के
स्थान विशेष में सन्निहित दिव्य शक्तियाँ हैं जिन्हें जाग्रत् करके विशिष्ट
क्षमता संपन्न बनाया जा सकता है।
ग्रांट मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापक वाई० जी० नाडगिर और एडगर जे० टामस ने
संयुक्त रूप से पुस्तक की भूमिका लिखते हुए कहा है कि वैदिक ऋषियों के
शरीरशास्त्र संबंधी गहन ज्ञान पर अचंभा होता है कि उस साधन हीन समय में किस
प्रकार उन्होंने इतनी गहरी जानकारियाँ प्राप्त की होंगी? आँख की सीप में ऊपर
के मस्तिष्क का भाग वृहत् मस्तिष्क कहलाता है। वही सेरिबेलम-ब्रह्म चेतना
शक्ति का केंद्र है, इंद्र और सविता यहीं निवास करते हैं। नाक की सीध में सिर
के पीछे वाला भाग-सेरिबेलम–अनुमस्तिष्क-रुद्र और पूषन देवता का कार्य क्षेत्र
है, मस्तिष्क का ऊपरी भाग-रोदसी, मध्य भाग अंतरिक्ष और निम्न भाग पृथ्वी
बतलाया गया है। रोदसी से दिव्य चेतना का प्रवाह अंतरिक्ष में ग्रह-नक्षत्रों
वाला ब्रह्मांड और पृथ्वी से अपने लोक में काम कर रही भौतिक शक्तियों का
सूत्र संबंध जुड़ा रहता है। सप्तधार, सोम, वरुण, अग्नि, स्वर्ग द्वार, अत्रि,
द्रोण, कलश एवं अश्विनी शक्तियों का संबंध रोदसी क्षेत्र से है।
अग्नि से नीचे वाले भाग को स्वर्ग द्वार और उससे नीचे वाले भाग को द्रोण कलश
कहा गया है, जहाँ से सप्तसरिताएँ–सात नदियाँ बहती हैं। द्रोण कलश में सोमरस
भरा रहता है, जिसके आधार पर स्नायु केंद्रों को शक्ति प्राप्त होती है।
मेरुरज्जुओं के साथ बँधे हुए दो ग्रंथि गुच्छक अश्विनीकुमार बताये गये हैं।
मस्तिष्क की परिधि को घेरे हुए एक विशेष द्रव संपूर्ण मस्तिष्क को चेतना
प्रदान करता है, इसी को वरुण कहते हैं। इसी केंद्र में अग्नि देवता का
ज्ञानकोष है। मस्तिष्क के पिछले भाग में अवस्थित "टेंपोलर लोव" प्राचीन काल
का शंख पालि है। इसके नीचे की पीयूष ग्रंथियाँ जिन्हें मेडुला भी कहते हैं,
अश्वमेध यज्ञ की वेदी है। अश्वमेध अर्थात् इंद्रिय परिष्कार इसके लिए पीयूष
ग्रंथि वाला क्षेत्र ही उत्तरदायी है।
देवताओं की चमत्कारी शक्तियों का साधना विज्ञान के अंतर्गत विस्तृत वर्णन
किया गया है, वस्तुतः वह अपने भीतर मस्तिष्कीय क्षेत्र में सन्निहित दिव्य
शक्तियाँ हैं, जिन्हें अनुकूल बनाकर वे सभी ऋद्धि-सिद्धियों के रूप के कहे
समझे जाते हैं।
|
|||||