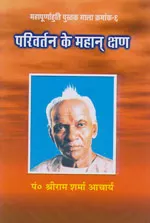|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> परिवर्तन के महान् क्षण परिवर्तन के महान् क्षणश्रीराम शर्मा आचार्य
|
62 पाठक हैं |
||||||
उज्जवल भविष्य की संरचना...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
परिवर्तन के महान् क्षण
बीसवीं सदी का अन्त आते-आते समय सचमुच बदल गया है। कभी
संवेदनाएँ
इतनी समर्थता प्रकट करती थीं कि मिट्टी के द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुष
विद्या में प्रवीण-पारंगत कर दिया करते थे। मीरा के कृष्ण उसके बुलाते ही
साथ नृत्य करने आ पहुँचते थे। गान्धारी ने पतिव्रत भावना से प्रेरित होकर
आँखों में पट्टी बाँध ली थी और आँखों में इतना प्रभाव भर लिया था कि
दृष्टिपात करते ही दुर्योधन का शरीर अष्ट-धातु का हो गया था। तब शाप-वरदान
भी शस्त्र प्रहारों और बहुमूल्य उपहारों जैसा काम करते थे। वह
भाव-संवेदनाओं का चमत्कार था। उसे एक सच्चाई के रूप में देखा और हर कसौटी
पर सही पाया जाता था।
अब भौतिक जगत ही सब कुछ रह गया है। आत्मा तिरोहित हो गयी है। शरीर और विलास-वैभव ही सब कुछ बनकर रह गए हैं। यह प्रत्यक्षवाद है। जो बाजीगरों की तरह हाथों में देखा और दिखाया जा सके वही सच और जिसके लिए गहराई में उतरना पड़े, परिणाम के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, वह झूठ। आत्मा दिखाई नहीं देती। परमात्मा को भी अमुक शरीर धारण किए, अमुक स्थान पर बैठा हुआ और अमुक हलचलें करते नहीं देखा जाता इसलिए उन दोनों की ही मान्यता समाप्त कर दी गयी।
भौतिक विज्ञान चूँकि प्रत्यक्ष पर अवलम्बित है। उतने को ही सच मानता है जो प्रत्यक्ष देखा जाता है। चेतना और श्रद्धा में कभी शक्ति की मान्यता रही होगी, पर वह अब इसलिए अविश्वस्त हो गयी कि उन्हें बटन दबाते ही बिजली जल जाने या पंखा चलने लगने की तरह प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। जो प्रत्यक्ष नहीं वह अमान्य, भौतिक विज्ञान और दर्शन की यह कसौटी है। इस आधार पर परिवर्तन का लाभ तो यह हुआ कि अन्ध-विश्वास जैसी मूढ़-मान्यताओं के लिए गुंजायश नहीं रही और हानि यह हुई कि नीतिमत्ता, आदर्शवादिता, धर्म-धारणाओं को भी अस्वीकार कर दिया गया। इस लिए मानवी गरिमा के अनुरूप अनुशासन भी लगभग समाप्त होने जा रहा है।
नई मान्यता के अनुसार मनुष्य एक चलता-फिरता पौधा मान लिया गया। अधिक से अधिक उसे वार्तालाप कर सकने की विशेषता वाला पशु माना जाने लगा। प्राणीवध में जिस निर्दयता, और निष्ठुरता का आरोपण कर लोग अनुचित और अधार्मिक माना करते थे, वह अब असमंजस का विषय नहीं रह सकेगा, ऐसा दीखता है। कद्दू-बैंगन की तरह किसी भी पशु-पक्षी को माँसाहार के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरे की पीड़ा जब हमें स्वयं को अनुभव नहीं होती और सामिष आहार के अधिक प्रोटीन होने और अपने शरीर को लाभ मिलने की बात प्रत्यक्षवादी कहने लगें तो कोई प्राणीवध को इसलिए क्यों अस्वीकार करे कि उसके कारण नीति का अनुशासन बिगड़ता है तथा भावनाएँ विचलित होती हैं। ठीक यही बात अन्य मानवी मर्यादाओं के संबंध में भी हैं। अपराधों के लिए द्वार इसीलिए खुला कि उसमें मात्र दूसरों की हानि होती है। अपने को तत्काल लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है, अन्य विचारों में भी पशु-प्रवृत्तियों को अपनाए जाने के संबंध में जो तर्क दिए गए और प्रतिपादन प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें देखते हुए यौन सदाचार के लिए भी किसी पर कोई दबाव नहीं पड़ता। जब इस संबंध में पशु सर्वथा स्वतंत्र हैं तो मनुष्य के लिए ही क्यों इस संदर्भ में प्रतिबंध होना चाहिए। जीव-जगत में जब धर्म, कर्त्तव्य, दायित्व जैसी कोई मान्यता नहीं तो फिर मनुष्य ही उन जंजालों में अपने को क्यों बांधे ? जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, जब बड़ी चिड़िया को छोटी चिड़ियों पर आक्रमण करने में कोई हिचक नहीं होती, जब चीते हिरन स्तर के कमजोरों को दबोच लेते हैं तो फिर समर्थ मनुष्य ही अपने असमर्थ जनों का शोषण करने में क्यों चूके ?
प्रत्यक्षवाद ने, भौतिक विज्ञान ने सुविधा-संवर्धन के लिए कितने ही नये-नये आधार दिए हैं, तो उसकी उपयोगिता और यथार्थता पर क्या किसी को संदेह करना चाहिए। यदि आत्मा, परमात्मा, कर्म, कर्त्तव्य, पुण्य, परमार्थ जैसी मान्यताओं के आधार पर कोई लाभ हाथों-हाथ नहीं मिलता तो फिर व्यर्थ ही उन बंधनों को क्यों माना जाए, जिनके कारण अपने के तो तात्कालिक घाटे में ही रहना पड़ता है। समर्थों को इसके कारण संत्रस्त और शोषण का शिकार बनना पड़ता है।
अब भौतिक जगत ही सब कुछ रह गया है। आत्मा तिरोहित हो गयी है। शरीर और विलास-वैभव ही सब कुछ बनकर रह गए हैं। यह प्रत्यक्षवाद है। जो बाजीगरों की तरह हाथों में देखा और दिखाया जा सके वही सच और जिसके लिए गहराई में उतरना पड़े, परिणाम के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, वह झूठ। आत्मा दिखाई नहीं देती। परमात्मा को भी अमुक शरीर धारण किए, अमुक स्थान पर बैठा हुआ और अमुक हलचलें करते नहीं देखा जाता इसलिए उन दोनों की ही मान्यता समाप्त कर दी गयी।
भौतिक विज्ञान चूँकि प्रत्यक्ष पर अवलम्बित है। उतने को ही सच मानता है जो प्रत्यक्ष देखा जाता है। चेतना और श्रद्धा में कभी शक्ति की मान्यता रही होगी, पर वह अब इसलिए अविश्वस्त हो गयी कि उन्हें बटन दबाते ही बिजली जल जाने या पंखा चलने लगने की तरह प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। जो प्रत्यक्ष नहीं वह अमान्य, भौतिक विज्ञान और दर्शन की यह कसौटी है। इस आधार पर परिवर्तन का लाभ तो यह हुआ कि अन्ध-विश्वास जैसी मूढ़-मान्यताओं के लिए गुंजायश नहीं रही और हानि यह हुई कि नीतिमत्ता, आदर्शवादिता, धर्म-धारणाओं को भी अस्वीकार कर दिया गया। इस लिए मानवी गरिमा के अनुरूप अनुशासन भी लगभग समाप्त होने जा रहा है।
नई मान्यता के अनुसार मनुष्य एक चलता-फिरता पौधा मान लिया गया। अधिक से अधिक उसे वार्तालाप कर सकने की विशेषता वाला पशु माना जाने लगा। प्राणीवध में जिस निर्दयता, और निष्ठुरता का आरोपण कर लोग अनुचित और अधार्मिक माना करते थे, वह अब असमंजस का विषय नहीं रह सकेगा, ऐसा दीखता है। कद्दू-बैंगन की तरह किसी भी पशु-पक्षी को माँसाहार के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरे की पीड़ा जब हमें स्वयं को अनुभव नहीं होती और सामिष आहार के अधिक प्रोटीन होने और अपने शरीर को लाभ मिलने की बात प्रत्यक्षवादी कहने लगें तो कोई प्राणीवध को इसलिए क्यों अस्वीकार करे कि उसके कारण नीति का अनुशासन बिगड़ता है तथा भावनाएँ विचलित होती हैं। ठीक यही बात अन्य मानवी मर्यादाओं के संबंध में भी हैं। अपराधों के लिए द्वार इसीलिए खुला कि उसमें मात्र दूसरों की हानि होती है। अपने को तत्काल लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है, अन्य विचारों में भी पशु-प्रवृत्तियों को अपनाए जाने के संबंध में जो तर्क दिए गए और प्रतिपादन प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें देखते हुए यौन सदाचार के लिए भी किसी पर कोई दबाव नहीं पड़ता। जब इस संबंध में पशु सर्वथा स्वतंत्र हैं तो मनुष्य के लिए ही क्यों इस संदर्भ में प्रतिबंध होना चाहिए। जीव-जगत में जब धर्म, कर्त्तव्य, दायित्व जैसी कोई मान्यता नहीं तो फिर मनुष्य ही उन जंजालों में अपने को क्यों बांधे ? जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, जब बड़ी चिड़िया को छोटी चिड़ियों पर आक्रमण करने में कोई हिचक नहीं होती, जब चीते हिरन स्तर के कमजोरों को दबोच लेते हैं तो फिर समर्थ मनुष्य ही अपने असमर्थ जनों का शोषण करने में क्यों चूके ?
प्रत्यक्षवाद ने, भौतिक विज्ञान ने सुविधा-संवर्धन के लिए कितने ही नये-नये आधार दिए हैं, तो उसकी उपयोगिता और यथार्थता पर क्या किसी को संदेह करना चाहिए। यदि आत्मा, परमात्मा, कर्म, कर्त्तव्य, पुण्य, परमार्थ जैसी मान्यताओं के आधार पर कोई लाभ हाथों-हाथ नहीं मिलता तो फिर व्यर्थ ही उन बंधनों को क्यों माना जाए, जिनके कारण अपने के तो तात्कालिक घाटे में ही रहना पड़ता है। समर्थों को इसके कारण संत्रस्त और शोषण का शिकार बनना पड़ता है।
विज्ञान और प्रत्यक्षवाद ने क्या सचमुच हमें सुखी बनाया है ?
समय का बदलाव, वैज्ञानिक उपलब्धियों तक तर्क के आधार पर प्रदर्शन करने के
रूप में जब लाभदायक प्रतीत है तो उसके स्थान पर तप, संयम, परमार्थ जैसी उन
मान्यताओं को क्यों स्वीकार कर लिया जाय, जो आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं
धार्मिकता की दृष्टि से कितनी ही सराही क्यों न जाती हो पर तात्कालिक लाभ
की कसौटी पर उनके कारण घाटे में ही रहना पड़ता है।
नये समय के नये तर्क अपराधियों स्वेच्छाचारियों से लेकर हवा के साथ बहने वाले मनीषियों तक को समान रूप से अनुकूल पड़ते है। और मान्यता के रूप में अंगीकार करने में भी सुविधाजनक प्रतीत होते हैं तो हर कोई उसी को स्वीकार क्यों न करे ? उसी दिशा में क्यों न चलें ? मनीषी नीत्से ने दृढ़तापूर्वक घोषणा की है कि ‘‘तर्क के इस युग में पुरानी मान्यताओं पर आधारित ईश्वर मर चुका। अब उसे इतना गहरा दफना दिया गया है कि भविष्य में कभी उसके जीवित होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।’’ धर्म के सम्बन्ध में प्रत्यक्षवादी बौद्धिक बहुमत ने यही कहा है कि वह अफीम की गोली भर है, जो पिछड़ों को त्रास सहते और विपन्नता के विरुद्ध मुंह न खोलने के लिए बाधित करता है, साथ ही वह अनाचरियों को निर्भय बनाता है। ताकि लोक में अपनी चतुरता और समर्थता के बल पर वे उन कार्यो को करते रहें, जिन्हें अन्यान्य कहा जाता है। परलोक का प्रश्न यदि आड़े आता है तो वहाँ से बच निकलना और भी सरल है। किसी देवी-देवता की पूजा-पत्री कर देने या धार्मिक कर्मकाण्ड का सस्ता-सा आडंबर बना देने भर से पाप-कर्मों के दंड से सहज छुटकारा मिल जाता है। जब इतने सस्ते में तथाकथित पापों की प्रतिक्रिया से बचा जा सकता है। तो रास्ता बिलकुल साफ है। मौज से मनमानी करते रहा जा सकता है और उससे कोई कठोर प्रतिफल की आशंका हो तो पूजा-पाठ के सस्ते से खेल-खिलवाड़ करने से वह आशंका भी निरस्त हो सकती है।
समय का प्रवाह वैज्ञानिक प्रगति के साथ प्रत्यक्षवाद का सार्थक होता जा रहा है। सच तो यह है कि जो लोग धर्म और अध्यात्म को चर्चा-प्रसंगो में मान्यता देते हैं, वे भी निजी जीवन में प्रायः वैसे ही आचरण करते देखे जाते हैं जैसे कि अधर्मी और नास्तिक करते देखे जाते है। धर्मोपदेशक से लेकर धर्मध्वजियों के निजी जीवन का निरीक्षण करने पर प्रतीत होता है कि अधिकांश लोग उस स्वार्थपरता को ही अपनाये रहते हैं जो अधार्मिकता की परिधि में आती है। आडंबर, पाखण्ड और प्रपंच एक प्रकार से प्रच्छन्न की महत्ता भी बखानते हैं, अन्यथा जो आस्तिकता और धार्मिकता की महत्ता भी बखानते हैं, उन्हें स्वयं तो भीतर बाहर में से एक होना ही चाहिए था। जब उनकी स्थिति आडंबर भरी होती दीखती है, तो प्रतीत होता है कि प्रत्यक्षवादी नास्तिता ही नहीं प्रच्छन्न धर्माडंबर भी लगभग उसी मान्यता को अपनाये हुए हैं, लोगों की आँखों में धूल झोंकने या अनुचित लाभ उठाने के लिए ही धर्म का ढकोसला गले से बाँधा जा रहा है। ईश्वर को भी वे न्यायकारी-सर्वव्यापी नहीं मानते। यदि ऐसा होता तो धार्मिकता की वकालत करने वालों में से कोई भी परोक्ष रूप से अवांछनीयता अपनाये रहने के लिए तैयार नहीं होता। तथाकथित धार्मिक और खुलकर इंकार करने वाले लगभग एक ही स्तर के बन जाते हैं।
यह स्थिति भयानक है। वस्तओं की जिस कमी को विज्ञान को पूरा किया है यदि वह हस्तगत न हुई होती तो पिछली पीढ़ियों की तरह सदा जीवन अपनाकर भी निर्वाह हँसी-खुशी के साथ चलता रह सकता था। ऋषियों, तपश्वियों, महामानवों, लोक सेवियों में से अधिकांश ने कठिनाईयों और अभाव वाला भौतिक जीवन जिया है, फिर भी उनकी भौतिक या आध्यात्मिक स्थिति खिन्न, विपन्न नहीं रही। सच तो यह है कि वे आज के तथाकथित सुखी सृमृद्ध लोगों की तुलना में कहीं अधिक सुख-शांति भरा प्रगतिशील जीवन जीते थे और हँसता-हँसाता ऐसा वातावरण बनाये रखते थे, जिसे सतयुग के रूप में जाना जाता था और जिसको पुनः प्राप्त करने के लिए हम सब तरसते हैं।
भौतिक विज्ञान के सुविधा-साधन बढ़ाने वाले पक्ष ने समर्थ जनों के लिए लाभ उठाने के अनेकों आधार उत्पन्न एवं उपस्थित किये हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बहिरंग की इसी स्तर की चमक-दमक को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि विज्ञान ने अपने समय को बहुत सुविधा-सम्पन्न बनाया है। परन्तु दूसरी ओर तनिक-सी दृष्टि मोड़ते ही पर्दा उलट जाता है और दृश्य ठीक विपरीत दीखने लगता है। सुसपन्न समर्थ दस। विज्ञान द्वारा उत्पादित कम हैं। सामग्री में से अधिकांश उन्हीं के हाथों में सीमित होकर रह गयी है। उन्होंने जो बटोरा है वह भी कहीं आसमान से नहीं टपका वरन दुर्बल दीख पड़ने वाले भोले भावुकों को पिछड़े हुए समझकर उन्हीं के हाथों एकत्रित हुई है। जिसे विज्ञान की देन, युग का आभाव, प्रगति का युग आदि नामों से श्रेय दिया जाता है। इस एक पक्ष की बढ़ोत्तरी ने अधिकांश लोगों का बडी मात्रा में दोहन किस प्रकार किया है। इसे देखते हुए विवेकवानों को उस असमंजस में डूबना पड़ता है कि दृष्टिगोचर होने वाली प्रगति क्या वास्तविक प्रगति है ? इसके पीछे अधिकांश को पीड़ित शोषित, अभावग्रस्त रखने वाला कुचक्र तो काम नहीं कर रहा है।
नये समय के नये तर्क अपराधियों स्वेच्छाचारियों से लेकर हवा के साथ बहने वाले मनीषियों तक को समान रूप से अनुकूल पड़ते है। और मान्यता के रूप में अंगीकार करने में भी सुविधाजनक प्रतीत होते हैं तो हर कोई उसी को स्वीकार क्यों न करे ? उसी दिशा में क्यों न चलें ? मनीषी नीत्से ने दृढ़तापूर्वक घोषणा की है कि ‘‘तर्क के इस युग में पुरानी मान्यताओं पर आधारित ईश्वर मर चुका। अब उसे इतना गहरा दफना दिया गया है कि भविष्य में कभी उसके जीवित होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।’’ धर्म के सम्बन्ध में प्रत्यक्षवादी बौद्धिक बहुमत ने यही कहा है कि वह अफीम की गोली भर है, जो पिछड़ों को त्रास सहते और विपन्नता के विरुद्ध मुंह न खोलने के लिए बाधित करता है, साथ ही वह अनाचरियों को निर्भय बनाता है। ताकि लोक में अपनी चतुरता और समर्थता के बल पर वे उन कार्यो को करते रहें, जिन्हें अन्यान्य कहा जाता है। परलोक का प्रश्न यदि आड़े आता है तो वहाँ से बच निकलना और भी सरल है। किसी देवी-देवता की पूजा-पत्री कर देने या धार्मिक कर्मकाण्ड का सस्ता-सा आडंबर बना देने भर से पाप-कर्मों के दंड से सहज छुटकारा मिल जाता है। जब इतने सस्ते में तथाकथित पापों की प्रतिक्रिया से बचा जा सकता है। तो रास्ता बिलकुल साफ है। मौज से मनमानी करते रहा जा सकता है और उससे कोई कठोर प्रतिफल की आशंका हो तो पूजा-पाठ के सस्ते से खेल-खिलवाड़ करने से वह आशंका भी निरस्त हो सकती है।
समय का प्रवाह वैज्ञानिक प्रगति के साथ प्रत्यक्षवाद का सार्थक होता जा रहा है। सच तो यह है कि जो लोग धर्म और अध्यात्म को चर्चा-प्रसंगो में मान्यता देते हैं, वे भी निजी जीवन में प्रायः वैसे ही आचरण करते देखे जाते हैं जैसे कि अधर्मी और नास्तिक करते देखे जाते है। धर्मोपदेशक से लेकर धर्मध्वजियों के निजी जीवन का निरीक्षण करने पर प्रतीत होता है कि अधिकांश लोग उस स्वार्थपरता को ही अपनाये रहते हैं जो अधार्मिकता की परिधि में आती है। आडंबर, पाखण्ड और प्रपंच एक प्रकार से प्रच्छन्न की महत्ता भी बखानते हैं, अन्यथा जो आस्तिकता और धार्मिकता की महत्ता भी बखानते हैं, उन्हें स्वयं तो भीतर बाहर में से एक होना ही चाहिए था। जब उनकी स्थिति आडंबर भरी होती दीखती है, तो प्रतीत होता है कि प्रत्यक्षवादी नास्तिता ही नहीं प्रच्छन्न धर्माडंबर भी लगभग उसी मान्यता को अपनाये हुए हैं, लोगों की आँखों में धूल झोंकने या अनुचित लाभ उठाने के लिए ही धर्म का ढकोसला गले से बाँधा जा रहा है। ईश्वर को भी वे न्यायकारी-सर्वव्यापी नहीं मानते। यदि ऐसा होता तो धार्मिकता की वकालत करने वालों में से कोई भी परोक्ष रूप से अवांछनीयता अपनाये रहने के लिए तैयार नहीं होता। तथाकथित धार्मिक और खुलकर इंकार करने वाले लगभग एक ही स्तर के बन जाते हैं।
यह स्थिति भयानक है। वस्तओं की जिस कमी को विज्ञान को पूरा किया है यदि वह हस्तगत न हुई होती तो पिछली पीढ़ियों की तरह सदा जीवन अपनाकर भी निर्वाह हँसी-खुशी के साथ चलता रह सकता था। ऋषियों, तपश्वियों, महामानवों, लोक सेवियों में से अधिकांश ने कठिनाईयों और अभाव वाला भौतिक जीवन जिया है, फिर भी उनकी भौतिक या आध्यात्मिक स्थिति खिन्न, विपन्न नहीं रही। सच तो यह है कि वे आज के तथाकथित सुखी सृमृद्ध लोगों की तुलना में कहीं अधिक सुख-शांति भरा प्रगतिशील जीवन जीते थे और हँसता-हँसाता ऐसा वातावरण बनाये रखते थे, जिसे सतयुग के रूप में जाना जाता था और जिसको पुनः प्राप्त करने के लिए हम सब तरसते हैं।
भौतिक विज्ञान के सुविधा-साधन बढ़ाने वाले पक्ष ने समर्थ जनों के लिए लाभ उठाने के अनेकों आधार उत्पन्न एवं उपस्थित किये हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बहिरंग की इसी स्तर की चमक-दमक को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि विज्ञान ने अपने समय को बहुत सुविधा-सम्पन्न बनाया है। परन्तु दूसरी ओर तनिक-सी दृष्टि मोड़ते ही पर्दा उलट जाता है और दृश्य ठीक विपरीत दीखने लगता है। सुसपन्न समर्थ दस। विज्ञान द्वारा उत्पादित कम हैं। सामग्री में से अधिकांश उन्हीं के हाथों में सीमित होकर रह गयी है। उन्होंने जो बटोरा है वह भी कहीं आसमान से नहीं टपका वरन दुर्बल दीख पड़ने वाले भोले भावुकों को पिछड़े हुए समझकर उन्हीं के हाथों एकत्रित हुई है। जिसे विज्ञान की देन, युग का आभाव, प्रगति का युग आदि नामों से श्रेय दिया जाता है। इस एक पक्ष की बढ़ोत्तरी ने अधिकांश लोगों का बडी मात्रा में दोहन किस प्रकार किया है। इसे देखते हुए विवेकवानों को उस असमंजस में डूबना पड़ता है कि दृष्टिगोचर होने वाली प्रगति क्या वास्तविक प्रगति है ? इसके पीछे अधिकांश को पीड़ित शोषित, अभावग्रस्त रखने वाला कुचक्र तो काम नहीं कर रहा है।
नीतिरहित भौतिकवाद से उपजी दुर्गति
ऊँचा महल खड़ा करने के लिए किसी दूसरी जगह गड्ढे बनाने पड़ते हैं। मिट्टी,
पत्थर, चूना आदि जमीन को खोदकर ही निकाला जाता है। एक जगह टीला बनता है तो
दूसरी जगह खाई बनती है। संसार में दरिद्रों, अशिक्षितों, दुःखियों,
पिछड़ों की विपुल संख्या देखते हुए विचार उठता है कि उत्पत्ति सम्पदा यदि
सभी में बँट गई होती तो सभी लोग लगभग एक ही तरह का सामान स्तर का जीवन जी
रहे होते है।
अभाव क्रमिक है। वह मात्र एक ही कारण उत्पन्न होता हुआ है कि कुछ लोगों ने अधिक बटोरने की विज्ञान एवं प्रत्यक्षवाद की विनिर्मित मान्यता के अनुरूप यह उचित समझा है कि नीति, धर्म, कर्तव्य, सदाशयता, शालीनता, समता, परमार्थ, परायणता जैसे उन अनुबंधों को मानने से इंकार कर दिया जाय जो पिछली पीढ़ियों में आस्तिकता और धार्मिकता के आधार पर आवश्यक माने जाते थे। अब उन्हें प्रत्यक्षवाद ने अमान्य ठहरा दिया तो सामर्थ्यवानों को कोई किस आदार पर मर्यादा में रहने के लिए समझाये ? किस तर्क के आधार पर शालीनता और समता की नीति अपनाने के लिए बाधित करे।
अभाव क्रमिक है। वह मात्र एक ही कारण उत्पन्न होता हुआ है कि कुछ लोगों ने अधिक बटोरने की विज्ञान एवं प्रत्यक्षवाद की विनिर्मित मान्यता के अनुरूप यह उचित समझा है कि नीति, धर्म, कर्तव्य, सदाशयता, शालीनता, समता, परमार्थ, परायणता जैसे उन अनुबंधों को मानने से इंकार कर दिया जाय जो पिछली पीढ़ियों में आस्तिकता और धार्मिकता के आधार पर आवश्यक माने जाते थे। अब उन्हें प्रत्यक्षवाद ने अमान्य ठहरा दिया तो सामर्थ्यवानों को कोई किस आदार पर मर्यादा में रहने के लिए समझाये ? किस तर्क के आधार पर शालीनता और समता की नीति अपनाने के लिए बाधित करे।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book