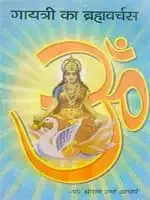|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> गायत्री का ब्रह्मवर्चस गायत्री का ब्रह्मवर्चसश्रीराम शर्मा आचार्य
|
314 पाठक हैं |
||||||
गायत्री को सर्वापरि क्यों मानते हैं
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
गायत्री उपासना से ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति
आत्मा में सन्निहित ब्रह्मवर्चस का जागरण करने के लिए गायत्री उपासना
आवश्यक है। यों सभी के भीतर सत्-तत्व बीज रूप में विद्यमान है पर उसका
जागरण जिन तपश्चर्याओं द्वारा सम्भव होता है, उनमें गायत्री उपासाना ही
प्रधान है। हर आस्तिक को अपने में ब्रह्म तेज उत्पन्न करना चाहिए। जिसमें
जितना ब्रह्म-तत्त्व अवतरित होगा, वह उतने ही अंशों में ब्राह्मणत्व का
अधिकारी होता जायेगा। जिसने आदर्शमय जीवन का व्रत लिया है, व्रतबंध,
यज्ञोपवीत धारण किया है, वे सभी व्रतधारी अपनी आत्मा में प्रकाश उत्पन्न
करने के लिए गायत्री उपासना निरन्तर करते रहें, यही उचित है। जो इस
कर्त्तव्य से च्युत होकर इधर-उधर भटकते हैं, जड़ की सींचना छोड़कर पत्ते
धोते फिरते हैं, उन्हें अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में विलम्ब ही नहीं,
असफलता का भी सामना करना पड़ता है।
साधना शास्त्रों में निष्ठावान भारतीय धर्मानुयायियों को, द्विजों को एक मात्र गायत्री उपासना का ही निर्देश किया गया है। उसमें वे अपना ब्रह्मवर्चस आशाजनक मात्रा में बढ़ा सकते हैं और उस आधार पर विपन्नता एवं आपत्तियों से बचाते सुख शान्ति के मार्ग पर सुनिश्चित गति से बढ़ते रह सकते हैं। द्विजत्व का व्रत-बंध स्वीकार करते समय हर व्यक्ति को गायत्री मन्त्र की दीक्षा लेनी पड़ती है, इसलिए उसे ही गुरुमन्त्र कहा जाता रहा है। पीछे से अन्धकार युग में चले सम्प्रदायवाद ने अनेक देवी-देवता, मंत्र और अनेक उपासना विधान गढ़ डाले और लोगों को निर्दिष्ट मार्ग से भटकाकर भ्रम-जंजालों में उलझा दिया। फलत: अनादि काल से प्रत्येक भारतीय धर्मानुयायी की निर्दिष्ट उपासना पद्धति हाथ से छूट गई और आधार रहित पतंग की तरह हम इधर उधर टकराते हुए अध:पतित स्थिति में जा पहुँचे।
शास्त्र कथन है-
साधना शास्त्रों में निष्ठावान भारतीय धर्मानुयायियों को, द्विजों को एक मात्र गायत्री उपासना का ही निर्देश किया गया है। उसमें वे अपना ब्रह्मवर्चस आशाजनक मात्रा में बढ़ा सकते हैं और उस आधार पर विपन्नता एवं आपत्तियों से बचाते सुख शान्ति के मार्ग पर सुनिश्चित गति से बढ़ते रह सकते हैं। द्विजत्व का व्रत-बंध स्वीकार करते समय हर व्यक्ति को गायत्री मन्त्र की दीक्षा लेनी पड़ती है, इसलिए उसे ही गुरुमन्त्र कहा जाता रहा है। पीछे से अन्धकार युग में चले सम्प्रदायवाद ने अनेक देवी-देवता, मंत्र और अनेक उपासना विधान गढ़ डाले और लोगों को निर्दिष्ट मार्ग से भटकाकर भ्रम-जंजालों में उलझा दिया। फलत: अनादि काल से प्रत्येक भारतीय धर्मानुयायी की निर्दिष्ट उपासना पद्धति हाथ से छूट गई और आधार रहित पतंग की तरह हम इधर उधर टकराते हुए अध:पतित स्थिति में जा पहुँचे।
शास्त्र कथन है-
ब्रह्मत्वं चेदाप्तुकामोऽस्युयास्व गायत्रीं चेल्लोककामेऽन्यदेवम् कामो
ज्ञात: क्चीय पाद प्रवृत्या वाद: को वा तृप्ति हीने प्रवृत्ति:।
बुद्ध: साक्षी बुद्धिगम्यो जयादौ गायत्र्यर्थ: साऽनघो वेद साम: तद ब्रह्मैव ब्रह्मतोपासकस्याप्येवं मन्त्र: कोऽस्ति तत्रे पुराणै।।13।।
जात्यश्व: किं जातिमाप्तुं सकामो गत्यभ्यासात्स्यष्टता मेति जाति:। ब्रह्मत्वाप्तौ क: प्रयासो द्विजा नां गायत्र्या व्यज्यते चाष्टमेऽब्दे।।14।।
ब्रह्मत्वस्य स्यापनार्थ प्रविष्टा गायत्रीयं तावतास्य द्विजत्वम्।
कर्ण द्वारा ब्रह्म जन्म प्रदानायुक्तो वेदे ब्राह्मणो ब्रह्मविष्ठ:।।16।।
बुद्ध: साक्षी बुद्धिगम्यो जयादौ गायत्र्यर्थ: साऽनघो वेद साम: तद ब्रह्मैव ब्रह्मतोपासकस्याप्येवं मन्त्र: कोऽस्ति तत्रे पुराणै।।13।।
जात्यश्व: किं जातिमाप्तुं सकामो गत्यभ्यासात्स्यष्टता मेति जाति:। ब्रह्मत्वाप्तौ क: प्रयासो द्विजा नां गायत्र्या व्यज्यते चाष्टमेऽब्दे।।14।।
ब्रह्मत्वस्य स्यापनार्थ प्रविष्टा गायत्रीयं तावतास्य द्विजत्वम्।
कर्ण द्वारा ब्रह्म जन्म प्रदानायुक्तो वेदे ब्राह्मणो ब्रह्मविष्ठ:।।16।।
अर्थ- यदि किसी को ब्रह्मत्व की प्राप्ति करने की इच्छा है तो उसको
वेदमाता गायत्री की ही उपासना करनी चाहिए। यदि किसी लोकविशेष को प्राप्त
करने की इच्छा हो तो अन्य देवों की उपासना करो। अपने चरणों में प्रवृत्ति
करने से ही हार्दिक कामना का ज्ञान हो जाता है। जो तृप्ति हीन होता है,
उसी की प्रवृत्ति होती है। इसमें कोई भी वाद नहीं है।
यह बुद्धि की साक्षी है। गायत्री का जो अर्थ है वह अर्थ रहित, अर्थ पूर्ण पवित्र और वेदों का साररूप है, इसके जप आदि के करने में ही यह बुद्धि में गम्यमान होता है। ब्रह्मत्व प्राप्ति की जो उपासना करने वाला है, उसके लिए यह साक्षात् ब्रह्म ही है। गायत्री के समान मंत्र और पुराण में अन्य कोई भी मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र ही सर्व शिरोमणि मंत्र है।13।
जाति से जो अश्व है वह क्या कभी अपनी जाति की प्राप्ति करने की इच्छा वाला होता है ? उसकी जाति की स्पष्टता तो उसकी गति के अभ्यास से ही तुरन्त हो जाया करती है। इसी तरह ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए द्विजों का क्या प्रयास होता है, अर्थात् कुछ भी नहीं क्योंकि वह तो आठवें वर्ष में उपनयन संस्कार होने पर गायत्री माता के द्वारा स्वयं ही व्यज्यमान हो जाया करता है। ।।14।।
ब्रह्मत्व के स्थापना करने के लिए ही यह गायत्री प्रविष्ट होती है और तभी से द्विजत्व की इसके द्वारा प्राप्ति हुआ करती है। कानों में छिद्रों के द्वारा ब्रह्म जन्म का ज्ञान प्रदान किया जाता है अर्थात् गायत्री का उपदेश कानों में ही किया जाया करता है। जब दीक्षा-सम्पन्न होती है, तभी वह ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होता है, ऐसा ही वेदों में कहा गया है। ।।16।।
तात्पर्य यह है कि जन्मजात, ब्राह्मण कोई भी नहीं हो सकता है। यह तो मिथ्याभिमान ही होता है, क्योंकि ब्राह्मण का भले ही कोई पुत्र हो किन्तु वह ब्राह्मण एवं द्विज तब तक नहीं हो सकता है, जब तक उसे आठवें वर्ष में उपनयन संस्कार होने पर गायत्री की दीक्षा नहीं होती है। गायत्री मन्त्र ही ब्रह्मत्व प्रदान करने वाला होता है।
ब्रह्मवर्चस् गायत्री उपासना से ही उपलब्ध होता है। इस उपासना से देव तत्वों की मानव शरीर में निरन्तर वृद्धि होती रहती है और शक्तिशाली व्यक्ति देवत्व की महिमा, महत्ताओं को उसी जीवन में उपलब्ध कर लेता है। उसमें देवी विशेषताएँ प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगती हैं।
यह बुद्धि की साक्षी है। गायत्री का जो अर्थ है वह अर्थ रहित, अर्थ पूर्ण पवित्र और वेदों का साररूप है, इसके जप आदि के करने में ही यह बुद्धि में गम्यमान होता है। ब्रह्मत्व प्राप्ति की जो उपासना करने वाला है, उसके लिए यह साक्षात् ब्रह्म ही है। गायत्री के समान मंत्र और पुराण में अन्य कोई भी मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र ही सर्व शिरोमणि मंत्र है।13।
जाति से जो अश्व है वह क्या कभी अपनी जाति की प्राप्ति करने की इच्छा वाला होता है ? उसकी जाति की स्पष्टता तो उसकी गति के अभ्यास से ही तुरन्त हो जाया करती है। इसी तरह ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए द्विजों का क्या प्रयास होता है, अर्थात् कुछ भी नहीं क्योंकि वह तो आठवें वर्ष में उपनयन संस्कार होने पर गायत्री माता के द्वारा स्वयं ही व्यज्यमान हो जाया करता है। ।।14।।
ब्रह्मत्व के स्थापना करने के लिए ही यह गायत्री प्रविष्ट होती है और तभी से द्विजत्व की इसके द्वारा प्राप्ति हुआ करती है। कानों में छिद्रों के द्वारा ब्रह्म जन्म का ज्ञान प्रदान किया जाता है अर्थात् गायत्री का उपदेश कानों में ही किया जाया करता है। जब दीक्षा-सम्पन्न होती है, तभी वह ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होता है, ऐसा ही वेदों में कहा गया है। ।।16।।
तात्पर्य यह है कि जन्मजात, ब्राह्मण कोई भी नहीं हो सकता है। यह तो मिथ्याभिमान ही होता है, क्योंकि ब्राह्मण का भले ही कोई पुत्र हो किन्तु वह ब्राह्मण एवं द्विज तब तक नहीं हो सकता है, जब तक उसे आठवें वर्ष में उपनयन संस्कार होने पर गायत्री की दीक्षा नहीं होती है। गायत्री मन्त्र ही ब्रह्मत्व प्रदान करने वाला होता है।
ब्रह्मवर्चस् गायत्री उपासना से ही उपलब्ध होता है। इस उपासना से देव तत्वों की मानव शरीर में निरन्तर वृद्धि होती रहती है और शक्तिशाली व्यक्ति देवत्व की महिमा, महत्ताओं को उसी जीवन में उपलब्ध कर लेता है। उसमें देवी विशेषताएँ प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगती हैं।
सर्व देवमयो विप्रो ब्रह्म-विष्णु शिवात्मक:।।
ब्रह्म तेज: समुद्भूत: सदा: प्राकृतिको द्विज:।।
ब्राह्मणै र्भुज्यते यत्र तत्र भुङ्कते हरि: स्वयम्।
तत्र ब्रह्मा च रुद्रश्च खेचरा ऋषयो मुनि:।।
पितरो देवता: सर्वे भुज्जन्ते नात्र संशय:।
सर्व देव मयो विप्रस्तम्मात्तं नाव मानय।।
ब्रह्मणं च जननी वेद स्याग्निं श्रुतिं च गाम्।।
नित्य मिच्छन्ति ते देवा यजितुं कर्म भूमिषु।।
ब्रह्म तेज: समुद्भूत: सदा: प्राकृतिको द्विज:।।
ब्राह्मणै र्भुज्यते यत्र तत्र भुङ्कते हरि: स्वयम्।
तत्र ब्रह्मा च रुद्रश्च खेचरा ऋषयो मुनि:।।
पितरो देवता: सर्वे भुज्जन्ते नात्र संशय:।
सर्व देव मयो विप्रस्तम्मात्तं नाव मानय।।
ब्रह्मणं च जननी वेद स्याग्निं श्रुतिं च गाम्।।
नित्य मिच्छन्ति ते देवा यजितुं कर्म भूमिषु।।
अर्थ- ब्राह्मण सर्व देवमय और ब्रह्मा-विष्णु एवं शिव स्वरूप है। द्विजगण
यद्यपि प्राकृतिक अर्थात् पंतभूतमय ही होते हैं, तो भी गायत्री के ब्रह्म
तेज से उनकी उत्पत्ति होती है। जिस स्थान पर गायत्री के उपासक ब्राह्मण
भोजन किया करते हैं, वहाँ साक्षात् स्वयं हरि ही भोजन किया करते हैं, और
वहाँ पर ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र-खेचर-ऋषि-मुनि, पितर और देवता सभी भोजन करके
संतृप्त होते हैं इसमें संदेह नहीं है, ब्राह्मण जो सावित्री के परमोपासक
है, वे सर्वदेवमय होते हैं, इसलिए उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए।
देवगण सदा यही कामना किया करते हैं कि इस कर्मभूमि में ब्राह्मण वेदमाता
गायत्री-अग्नि-श्रुति और गौ इन सबकी नित्य पूजा होती रहनी चाहिए।
गायत्री उपासना की महान् महत्ता का यह प्रतिपादन भारतीय दर्शन और योग शास्त्रों में पग-पग पर मिलता है। इतने पर भी यह देखा गया है कि कई बार विधि-विधान का पालन करते हुए भी लोग गायत्री उपासना के वह लाभ प्राप्त नहीं कर पाते जिनका इस तरह उल्लेख मिलता है। उसका कारण होता है वातावरण का प्रभाव। यह सच है कि अनेक प्राणवान व्यक्ति अपनी तप साधना और संकल्प शक्ति से वातावरण को भी बदल डालते हैं। किन्तु सच यह भी है कि मनुष्य के विकास में वातावरण का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में होता है। उपासना चूँकि व्यक्ति के संस्कारों से संबंध रखती है और प्रत्येक वातावरण अच्छे-बुरे संस्कार समाहित रखता है अतएव गायत्री उपासना में तो स्थान और वातावरण का महत्व निश्चित ही बहुत अधिक होना चाहिए।
इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि जब कौरव पाण्डव युद्ध के लिए स्थान चयन की बात आई तो श्रीकृष्ण ने एक विशेष दूत नियुक्त किया सर्वत्र युद्धस्थल की छानबीन की। कुरुक्षेत्र में उसने परस्पर दो सगे भाइयों को युद्ध करते देखा यह घटना उसने श्रीकृष्ण को बताई। फलत: यही क्षेत्र युद्ध के लिए चुना गया, क्योंकि उन्हें संदेह था भावनाशील होने के कारण कहीं अर्जुन युद्ध का परित्याग न कर बैठे। श्रवण कुमार के बारे में भी ऐसी कथा प्रख्यात है। वह जब अपने माता-पिता को काँवर में लिए तीर्थाटन करा रहे थे तो एक स्थान ऐसा आया जहाँ उसने न केवल काँवर पटक दी अपितु अपने माता-पिता को कटु शब्द भी कहे। उस प्रदेश से आगे निकल जाने के बाद उसे अपने कथन पर पश्चाताप हुआ इसके पर उसके पिता ने सान्त्वना देते हुए समझाया कि इसमें श्रवण का कोई दोष नहीं यह स्थान मय दानव का था जिसने कभी अपने माता-पिता को यही बन्दी बनाकर मृत्यु के घाट उतार दिया था। कुन्ती के बारे में भी एक ऐसी घटना का उल्लेख पुराणों में मिलता है। भूमि के संस्कार एक तथ्य हैं इसे कोई भी पवित्र जलाशयों, देव मन्दिरों तथा शमशान घाट में जाकर स्वयं अनुभव कर सकता है।
कल्लू की मिट्टी सेवों के लिए प्रसिद्ध है अच्छी से अच्छी खाद, जल और मौसम पाकर भी वैसे सेव आज तक कहीं नहीं उगाये जा सके।
नागपुर के सन्तरे और भुसावल के से केले अन्यत्र नहीं मिलते। मुजफ्फरपुर, देहरादून लीचियों के लिए प्रसिद्ध है तो लखनऊ खरबूजों के लिए, मलीहाबाद और बनारस जैसे स्वादिष्ट आम दूसरी जगह कम मिलते हैं। दुधारू गायें सारे देश में मिलती हैं। किन्तु हरियाणा की गायों का कोई मुकाबला नहीं। कोहकाफ जैसा सौन्दर्य सारी दुनिया में उपलब्ध नहीं तो रूस का ही अजरबेजान क्षेत्र शत जीवन के लिए विश्व विख्यात है। जहाँ सौ वर्ष के पूर्व मृत्यु को वैसा ही आकस्मिक माना जाता है जैसे किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाये। यह सब वातावरण के प्रभाव और संस्कार हैं। उनसे प्रभावित हुए मनुष्य कभी रह नहीं सकता, आज की परिस्थितियाँ तो वैसे भी सर्वत्र संस्कार विहीन हो गई हैं सो प्रयत्न करते हुए भी कई बार गायत्री उपासनाओं का अभीष्ट फल नहीं मिल पाता। हरिद्वार में ब्रह्मवर्चस की स्थापना का उद्देश्य गायत्री की उच्चस्तरीय साधना के इच्छुकों के लिए वह सुयोग ही प्राप्त कराना है।
साधना की सफलता में स्थान, क्षेत्र व वातावरण का असाधारण महत्व है। विशिष्ट साधानाओं के लिए घर छोड़कर अन्यत्र उपयुक्त स्थान में जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि पुराने निवास स्थान का ढर्रा अभ्यस्त रहने से वैसी मन: स्थिति बन नहीं पाती जैसी महत्वपूर्ण साधनाओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। कुटुब्यों के, परिचित लोगों के साथ जुड़े हुए भले-बुरे संबंधों की पकड़ बनी रहती हैं। कामों का दबाव बना रहता है। रोग द्वेष उभरते रहते हैं। दिनचर्या बदलने पर कुटुम्बी तथा साथी विचित्रता अनुभव करते और उसमें विरोध खड़ा करते हैं। आहार और दिनचर्या बदलने में विग्रह उत्पन्न होता है। घरों के निवासी साथी जिस प्रकृति के होते हैं वैसा ही वातावरण छाया रहता है। यह सब अड़चने है जो महत्वपूर्ण साधनाओं की न तो व्यवस्था बनने दती हैं और न मन:स्थिति ही वैसी रह पाती है।
गायत्री उपासना की महान् महत्ता का यह प्रतिपादन भारतीय दर्शन और योग शास्त्रों में पग-पग पर मिलता है। इतने पर भी यह देखा गया है कि कई बार विधि-विधान का पालन करते हुए भी लोग गायत्री उपासना के वह लाभ प्राप्त नहीं कर पाते जिनका इस तरह उल्लेख मिलता है। उसका कारण होता है वातावरण का प्रभाव। यह सच है कि अनेक प्राणवान व्यक्ति अपनी तप साधना और संकल्प शक्ति से वातावरण को भी बदल डालते हैं। किन्तु सच यह भी है कि मनुष्य के विकास में वातावरण का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में होता है। उपासना चूँकि व्यक्ति के संस्कारों से संबंध रखती है और प्रत्येक वातावरण अच्छे-बुरे संस्कार समाहित रखता है अतएव गायत्री उपासना में तो स्थान और वातावरण का महत्व निश्चित ही बहुत अधिक होना चाहिए।
इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि जब कौरव पाण्डव युद्ध के लिए स्थान चयन की बात आई तो श्रीकृष्ण ने एक विशेष दूत नियुक्त किया सर्वत्र युद्धस्थल की छानबीन की। कुरुक्षेत्र में उसने परस्पर दो सगे भाइयों को युद्ध करते देखा यह घटना उसने श्रीकृष्ण को बताई। फलत: यही क्षेत्र युद्ध के लिए चुना गया, क्योंकि उन्हें संदेह था भावनाशील होने के कारण कहीं अर्जुन युद्ध का परित्याग न कर बैठे। श्रवण कुमार के बारे में भी ऐसी कथा प्रख्यात है। वह जब अपने माता-पिता को काँवर में लिए तीर्थाटन करा रहे थे तो एक स्थान ऐसा आया जहाँ उसने न केवल काँवर पटक दी अपितु अपने माता-पिता को कटु शब्द भी कहे। उस प्रदेश से आगे निकल जाने के बाद उसे अपने कथन पर पश्चाताप हुआ इसके पर उसके पिता ने सान्त्वना देते हुए समझाया कि इसमें श्रवण का कोई दोष नहीं यह स्थान मय दानव का था जिसने कभी अपने माता-पिता को यही बन्दी बनाकर मृत्यु के घाट उतार दिया था। कुन्ती के बारे में भी एक ऐसी घटना का उल्लेख पुराणों में मिलता है। भूमि के संस्कार एक तथ्य हैं इसे कोई भी पवित्र जलाशयों, देव मन्दिरों तथा शमशान घाट में जाकर स्वयं अनुभव कर सकता है।
कल्लू की मिट्टी सेवों के लिए प्रसिद्ध है अच्छी से अच्छी खाद, जल और मौसम पाकर भी वैसे सेव आज तक कहीं नहीं उगाये जा सके।
नागपुर के सन्तरे और भुसावल के से केले अन्यत्र नहीं मिलते। मुजफ्फरपुर, देहरादून लीचियों के लिए प्रसिद्ध है तो लखनऊ खरबूजों के लिए, मलीहाबाद और बनारस जैसे स्वादिष्ट आम दूसरी जगह कम मिलते हैं। दुधारू गायें सारे देश में मिलती हैं। किन्तु हरियाणा की गायों का कोई मुकाबला नहीं। कोहकाफ जैसा सौन्दर्य सारी दुनिया में उपलब्ध नहीं तो रूस का ही अजरबेजान क्षेत्र शत जीवन के लिए विश्व विख्यात है। जहाँ सौ वर्ष के पूर्व मृत्यु को वैसा ही आकस्मिक माना जाता है जैसे किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाये। यह सब वातावरण के प्रभाव और संस्कार हैं। उनसे प्रभावित हुए मनुष्य कभी रह नहीं सकता, आज की परिस्थितियाँ तो वैसे भी सर्वत्र संस्कार विहीन हो गई हैं सो प्रयत्न करते हुए भी कई बार गायत्री उपासनाओं का अभीष्ट फल नहीं मिल पाता। हरिद्वार में ब्रह्मवर्चस की स्थापना का उद्देश्य गायत्री की उच्चस्तरीय साधना के इच्छुकों के लिए वह सुयोग ही प्राप्त कराना है।
साधना की सफलता में स्थान, क्षेत्र व वातावरण का असाधारण महत्व है। विशिष्ट साधानाओं के लिए घर छोड़कर अन्यत्र उपयुक्त स्थान में जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि पुराने निवास स्थान का ढर्रा अभ्यस्त रहने से वैसी मन: स्थिति बन नहीं पाती जैसी महत्वपूर्ण साधनाओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। कुटुब्यों के, परिचित लोगों के साथ जुड़े हुए भले-बुरे संबंधों की पकड़ बनी रहती हैं। कामों का दबाव बना रहता है। रोग द्वेष उभरते रहते हैं। दिनचर्या बदलने पर कुटुम्बी तथा साथी विचित्रता अनुभव करते और उसमें विरोध खड़ा करते हैं। आहार और दिनचर्या बदलने में विग्रह उत्पन्न होता है। घरों के निवासी साथी जिस प्रकृति के होते हैं वैसा ही वातावरण छाया रहता है। यह सब अड़चने है जो महत्वपूर्ण साधनाओं की न तो व्यवस्था बनने दती हैं और न मन:स्थिति ही वैसी रह पाती है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book