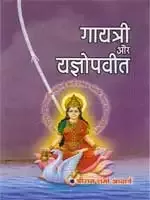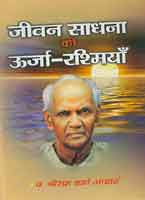|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> गायत्री और यज्ञोपवीत गायत्री और यज्ञोपवीतश्रीराम शर्मा आचार्य
|
42 पाठक हैं |
||||||
गायत्री और यज्ञोपवीत में क्या संबंध है
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
गायत्री और यज्ञोपवीत
यज्ञोपवीत की महान् उपयोगिता
यज्ञोपवीत का भारतीय धर्म में सर्वोपरि स्थान है। इसे द्विजत्व का प्रतीक
माना गया है। द्विजत्व का अर्थ है-मनुष्यता के उत्तरदायित्व को स्वीकार
करना। जो लोग मनुष्यता की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार नहीं,
पाशविक वृत्तियों में इतने जकड़े हुए हैं कि महान् मानवता का भार वहन नहीं
कर सकते, उनको ‘अनुपवीत’ शब्द से शास्त्रकारों ने
तिरस्कृत
किया है और उनके लिए आदेश किया है कि वे आत्मोन्नति करनेवाली मंडली से
अपने को पृथक्-बहिष्कृत समझें। ऐसे लोगों को वेद पाठ, यज्ञ, तप आदि
सत्साधनाओं का भी अनाधिकारी ठहराया गया है, क्योंकि जिसका आधार ही मजबूत
नहीं, वह स्वयं खड़ा नहीं रह सकता जब स्वयं खड़ा नहीं हो सकता, तो इन
धार्मिक कृत्यों का भार वहन किस प्रकार कर सकेगा ?
भारतीय धर्म-शास्त्रों की दृष्टि से मनुष्य का यह आवश्यक कर्त्तव्य है कि वह अनेक योनियों में भ्रमण करने के कारण संचित हुए पाशविक संस्कारों का परिमार्जन करके मनुष्योचित संस्कारों को धारण करे। इस धारणा को ही उन्होंने द्विजत्व के नाम से घोषित किया गया है। कोई व्यक्ति जन्म से ही द्विज नहीं होता, माता के गर्भ से तो सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं। शुभ संस्कारों को धारण करने से वे द्विज बनते हैं। महर्षि अत्रि का वचन है- ‘जन्मना जायते शूद्र: संस्कारात् द्विज उच्यते।’ जन्म-जात पाशविक संस्कारों को ही यदि कोई मनुष्य धारण किये रहे, तो उसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन की वृत्तियों में ही उलझा रहना पड़ेगा। कंचन-कामिनी से अधिक ऊँची कोई महत्त्वाकांक्षा उसके मन में न उठ सकेगी। इस स्थिति से ऊँचा उठना प्रत्येक मनुष्यताभिमानी के लिए आवश्यक है। इस आवश्यकता को ही हमारे प्रातः स्मरणीय ऋषियों ने अपने शब्दों में ‘उपवीत धारण करने की आवश्यकता’ बताया है।
किसी भी दृष्टि से विचार कीजिए, मनुष्य-जीवन की महत्ता सब प्रकार से असाधारण है। कहते हैं कि चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद नर-देह मिलती है, यदि इसे व्यर्थ गवाँ दिया जाय, तो पुनः कीट-पतंगों की चौरासी लाख योनियों में भटकने के लिए जाना पड़ता है। कहते हैं कि गर्भस्थ बालक जब रौरव नरक की यातना से दुःखी होकर भगवान् से छुटकारे की याचना करता है, तो इस शर्त पर छुटकारा मिलता है कि संसार में जाकर जीवन का सदुपयोग किया जायेगा। कहते हैं कि मनुष्य की रचना परमात्मा ने इस उद्देश्य से की है कि वह मेरा सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी राजकुमार सिद्ध हो और ऐसे कार्य करे, जो मेरी महिमा प्रकट करते हों। कहते हैं कि आत्मा का सर्वश्रेष्ठ विकास मानव प्राणी में होता है, इसलिए उसका आचरण ऐसा होना चाहिये, जिससे ईश्वर अंश जीव की महानता प्रकट हो।
हमारे पूर्वजों ने इस तथ्य को अपनी दूर-दृष्टि से, अपने योगबल से, पहले ही भली प्रकार समझ लिया था। उनने चिरकालीन विचार-मन्थन और सूक्ष्म दृष्टि से सृष्टि की प्रत्येक बात का गंभीर परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला था कि जन्म से मनुष्य भी पशु-पक्षियों के समान शिश्नोदर परायण होता है, पेट भरने और क्रीड़ा करने की इच्छायें उसे प्रधान रूप से सताती हैं, यदि कोई विशेष प्रयत्न करके उसे ऊँचा न उटाया जाय, तो वह कितना ही चतुर क्यों न कहलाये, पाश्विक वृत्तियों के आधार पर ही जीवन व्यतीत करेगा। चूँकि इस प्रकार की जीवनचर्या अत्यन्त ही तुच्छ और अदूरदर्शितापूर्ण है, इसलिए यही कल्याणकर है कि मनुष्यों को इस निम्न धरातल से ऊँचा उठकर उस भूमिका में अपना स्थान बनाना चाहिए, जो उच्च है, आदर्शपूर्ण है, धर्ममयी है और अनेक सत्परिणामों को उत्पन्न करनेवाली है। चूँकि यह स्थिति जन्म-जात पशु-वृत्तियों की क्रिया-शैली से बहुत भिन्न है, दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर है, इसलिए इस एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पदार्पण करने की परिवर्तन-पद्धति को ‘उपनयन’ कहा गया है।
देखने में यज्ञोपवीत कुछ लड़ों का एक सूत्र मात्र है, जो बायें कन्धे पर पड़ा रहता है। इसमें स्थूल रूप से कोई विशेषता नहीं मालूम पड़ती। बाजार में दो-दो, चार-चार आने के जनेऊ बिकते हैं। स्थूल दृष्टि से यही उसकी कीमत है तथा मोटे तौर से वह इस बात की पहचान है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों में से किसी वर्ण में इस जनेऊ पहनने वाले का जन्म हुआ है। पर वस्तुतः केवल मात्र इतना ही प्रयोजन उसका नहीं है। उसके पीछे एक जीवित-जागृत दर्शन-शास्त्र छिपा पड़ा है, जो मानव-जीवन का उत्तम रीति से गठन, निर्माण और विकास करता हुआ उस स्थान तक ले पहुँचता है, जो जीवधारी का चरम लक्ष्य है।
स्थूल दृष्टि से देखने में कई वस्तुयें बहुत ही साधारण प्रतीत होती हैं; पर उनका सूक्ष्म महत्त्व अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण होता है। पुस्तकें, स्थूल दृष्टि से देखने में छपे हुए कागजों का एक बण्डल मात्र है, जो रद्दी पर दो-चार पैसों की ठहरती है, पर उस पुस्तक में जो ज्ञान भरा हुआ है, वह इतना मूल्यवान् है कि उसके आधार पर मनुष्य कुछ से कुछ बन जाता है। ‘विक्टोरिया क्रास’ जो अंग्रेजी सरकार की ओर से बहादुरी का प्रतिष्ठित पदक दिया जाता था, वह लोहे का बना होता था और उसकी बाजारू कीमत मुश्किल से एकाध रुपया होगी, पर जो उसे प्राप्त कर लेता था, वह अपने आपको धन्य समझता था। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर जो प्रमाण-पत्र मिलते हैं उनके कागज का मूल्य एक-दो पैसे ही होगा पर वह कागज कितना मूल्यवान है- इसको वह परीक्षोत्तीर्ण छात्र ही जानता है। सरकारी कर्मचारियों के पद की पहचान के लिए धातु के बने अक्षर मिलते हैं, जो कि कन्धे या कपड़ों में लगा दिये जाते हैं। यह कर्मचारी जानते हैं कि उन्हें लगा लेने पर और उतार देने पर उनको जनता कितने अन्तर से पहचानती है। यज्ञोपवीत भी एक ऐसा ही प्रतीक है, जो बाजारू कीमत से भले ही कम हो; पर उसके पीछे एक महान् तत्त्वज्ञान जुड़ा हुआ है। इसलिये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जनेऊ पहनना कन्धे पर एक डोरा लटका लेना है, वरन् इस प्रकार सोचना चाहिए कि मनुष्य की दैवी जिम्मेदारियों का एक प्रतीक हमारे कन्धे पर अवस्थित है।
यह पूछा जाता है कि मन में कोई बात हो, तो उसी से सब कुछ हो सकता है, इसके लिये वाह्य-चिह्न धारण करने की क्या आवश्यकता है ? जब मन में द्विजत्व ग्रहण करने के भाव मौजूद हों, तो उसका होना ही पर्याप्त है। फिर यज्ञोपवीत क्यों पहनें ? और यदि मन में उस प्रकार की भावना नहीं है, तो जनेऊ पहनने से भी कुछ लाभ नहीं।
मोटे तौर से तर्क ठीक प्रतीत होता है, परन्तु जिन्होंने मनुष्य की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि इस तर्क में कितना कम तथ्य है। बुराई की ओर, अधर्म की ओर, पाशविक भोगों की ओर, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस ओर मन अपने आप चलता है, पर उसे त्याग के, संयम के, धर्म के मार्ग पर चलने के लिये बड़े-बड़े कष्ट साध्य प्रयत्न करने पड़ते हैं। पानी को बहाया जाय, तो वह जिधर नीची भूमि होगी, वह बिना किसी प्रयत्न के अपने आप अपना रास्ता बनाता हुआ बहेगा। निचाई जितना अधिक होगी, उतना ही पानी का बहाव तेज होता जायेगा, परन्तु यदि पानी को ऊपर चढ़ाना है, तो यह कार्य अपने आप नहीं हो सकता, इसके लिये तरह-तरह के साधन जुटाने पड़ेंगे। नल, पम्प, टंकी, आदि का कोई माध्यम लगाकर उसके पीछे ऐसी शक्ति का संयोग करना पड़ता है, जिसके दबाव से पानी ऊपर चढ़े। दबाव वाली शक्ति तथा पानी को ऊपर ले जाने वाले साधन यदि अच्छे हुए तो, वह तेजी से और अधिक मात्रा में ऊपर चढ़ता है, यदि वह साधन निर्बल हुए तो पानी चढ़ने की गति मन्द हो जायेगी।
यही बात जीव को उच्च मार्ग में लगाने के संबंध में भी है। यदि धर्म-मार्ग में, सिद्धान्तमय उच्चपथ में प्रगति करनी है, तो उसके लिए ऐसे प्रयत्न करने पड़ते हैं, जैसे कि पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए करने पड़ते हैं। सोलह संस्कार, नाना प्रकार के धार्मिक कर्म-काण्ड, व्रत, जप, पूजा, अनुष्ठान, तीर्थयात्रा, दान-पुण्य, स्वाध्याय, सत्संग ऐसे ही प्रयोजन हैं, जिसके द्वारा मन को प्रभावित, अभ्यस्त और संस्कृत बनाकर दिव्यत्व की ओर- द्विजत्व की ओर- बढ़ाया जाता है। इन सबका उद्देश्य मात्र केवल इतना ही है कि मन पाशविक वृत्तियों से मुड़कर दिव्यत्व की ओर अग्रसर हो, यदि ऐसा करना अपने आप ही सरलतापूर्वक हुआ तो यज्ञोपवीत को व्यर्थ बताने वाले तक को स्वीकार करने में किसी को कुछ आपत्ति न होगी। उस दिशा में यह पृथ्वी ब्रह्मलोक होती और वैसा समय सतयुग कहा जाता। पर आज तो वैसा नहीं है। हमारे मनों की कुटिलता इतनी बढ़ी हुई है कि आध्यात्मिक साधना करने वाले भी बार-बार भ्रष्ट हो जाते हैं, तब ऐसी आशा रखना कहा तक उचित है कि अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जायेगा।
यज्ञोपवीत धारण करना इसलिए आवश्यक है कि इससे एक प्रेरणा नियमित रूप से मिलती है। जिनके जिम्मे संसार के बड़े-बड़े कार्य हैं, जिनका जीवन व्यवस्थित है, वे सबेरे ही अपना कार्यक्रम बनाकर मेज के सामने लटका लेते हैं और उस तख्ती पर बार-बार निगाह डालकर अपने कार्यक्रम को यथोचित बनाते रहते हैं। यदि वह याद दिलाने वाली तख्ती न हो, तो उनके कार्यक्रम में गड़बड़ पड़ सकती है। यद्यपि उस तख्ती का स्वतः कोई बड़ा मूल्य नहीं है, पर उसके आधार पर काम करने वाले का अमूल्य समय व्यवस्थित रहता है। इसलिए उसका लाभ असाधारण महत्त्वपूर्ण है और उस महान् लाभ का श्रेय उस तख्ती को कम नहीं है। जनेऊ ऐसी ही एक तख्ती है, जो हमारे जीवनोद्देश्य और जीवन-क्रम को व्यवस्थित रखने की याद हर घड़ी दिलाती रहती है।
भारतीय धर्म-शास्त्रों की दृष्टि से मनुष्य का यह आवश्यक कर्त्तव्य है कि वह अनेक योनियों में भ्रमण करने के कारण संचित हुए पाशविक संस्कारों का परिमार्जन करके मनुष्योचित संस्कारों को धारण करे। इस धारणा को ही उन्होंने द्विजत्व के नाम से घोषित किया गया है। कोई व्यक्ति जन्म से ही द्विज नहीं होता, माता के गर्भ से तो सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं। शुभ संस्कारों को धारण करने से वे द्विज बनते हैं। महर्षि अत्रि का वचन है- ‘जन्मना जायते शूद्र: संस्कारात् द्विज उच्यते।’ जन्म-जात पाशविक संस्कारों को ही यदि कोई मनुष्य धारण किये रहे, तो उसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन की वृत्तियों में ही उलझा रहना पड़ेगा। कंचन-कामिनी से अधिक ऊँची कोई महत्त्वाकांक्षा उसके मन में न उठ सकेगी। इस स्थिति से ऊँचा उठना प्रत्येक मनुष्यताभिमानी के लिए आवश्यक है। इस आवश्यकता को ही हमारे प्रातः स्मरणीय ऋषियों ने अपने शब्दों में ‘उपवीत धारण करने की आवश्यकता’ बताया है।
किसी भी दृष्टि से विचार कीजिए, मनुष्य-जीवन की महत्ता सब प्रकार से असाधारण है। कहते हैं कि चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद नर-देह मिलती है, यदि इसे व्यर्थ गवाँ दिया जाय, तो पुनः कीट-पतंगों की चौरासी लाख योनियों में भटकने के लिए जाना पड़ता है। कहते हैं कि गर्भस्थ बालक जब रौरव नरक की यातना से दुःखी होकर भगवान् से छुटकारे की याचना करता है, तो इस शर्त पर छुटकारा मिलता है कि संसार में जाकर जीवन का सदुपयोग किया जायेगा। कहते हैं कि मनुष्य की रचना परमात्मा ने इस उद्देश्य से की है कि वह मेरा सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी राजकुमार सिद्ध हो और ऐसे कार्य करे, जो मेरी महिमा प्रकट करते हों। कहते हैं कि आत्मा का सर्वश्रेष्ठ विकास मानव प्राणी में होता है, इसलिए उसका आचरण ऐसा होना चाहिये, जिससे ईश्वर अंश जीव की महानता प्रकट हो।
हमारे पूर्वजों ने इस तथ्य को अपनी दूर-दृष्टि से, अपने योगबल से, पहले ही भली प्रकार समझ लिया था। उनने चिरकालीन विचार-मन्थन और सूक्ष्म दृष्टि से सृष्टि की प्रत्येक बात का गंभीर परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला था कि जन्म से मनुष्य भी पशु-पक्षियों के समान शिश्नोदर परायण होता है, पेट भरने और क्रीड़ा करने की इच्छायें उसे प्रधान रूप से सताती हैं, यदि कोई विशेष प्रयत्न करके उसे ऊँचा न उटाया जाय, तो वह कितना ही चतुर क्यों न कहलाये, पाश्विक वृत्तियों के आधार पर ही जीवन व्यतीत करेगा। चूँकि इस प्रकार की जीवनचर्या अत्यन्त ही तुच्छ और अदूरदर्शितापूर्ण है, इसलिए यही कल्याणकर है कि मनुष्यों को इस निम्न धरातल से ऊँचा उठकर उस भूमिका में अपना स्थान बनाना चाहिए, जो उच्च है, आदर्शपूर्ण है, धर्ममयी है और अनेक सत्परिणामों को उत्पन्न करनेवाली है। चूँकि यह स्थिति जन्म-जात पशु-वृत्तियों की क्रिया-शैली से बहुत भिन्न है, दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर है, इसलिए इस एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पदार्पण करने की परिवर्तन-पद्धति को ‘उपनयन’ कहा गया है।
देखने में यज्ञोपवीत कुछ लड़ों का एक सूत्र मात्र है, जो बायें कन्धे पर पड़ा रहता है। इसमें स्थूल रूप से कोई विशेषता नहीं मालूम पड़ती। बाजार में दो-दो, चार-चार आने के जनेऊ बिकते हैं। स्थूल दृष्टि से यही उसकी कीमत है तथा मोटे तौर से वह इस बात की पहचान है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों में से किसी वर्ण में इस जनेऊ पहनने वाले का जन्म हुआ है। पर वस्तुतः केवल मात्र इतना ही प्रयोजन उसका नहीं है। उसके पीछे एक जीवित-जागृत दर्शन-शास्त्र छिपा पड़ा है, जो मानव-जीवन का उत्तम रीति से गठन, निर्माण और विकास करता हुआ उस स्थान तक ले पहुँचता है, जो जीवधारी का चरम लक्ष्य है।
स्थूल दृष्टि से देखने में कई वस्तुयें बहुत ही साधारण प्रतीत होती हैं; पर उनका सूक्ष्म महत्त्व अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण होता है। पुस्तकें, स्थूल दृष्टि से देखने में छपे हुए कागजों का एक बण्डल मात्र है, जो रद्दी पर दो-चार पैसों की ठहरती है, पर उस पुस्तक में जो ज्ञान भरा हुआ है, वह इतना मूल्यवान् है कि उसके आधार पर मनुष्य कुछ से कुछ बन जाता है। ‘विक्टोरिया क्रास’ जो अंग्रेजी सरकार की ओर से बहादुरी का प्रतिष्ठित पदक दिया जाता था, वह लोहे का बना होता था और उसकी बाजारू कीमत मुश्किल से एकाध रुपया होगी, पर जो उसे प्राप्त कर लेता था, वह अपने आपको धन्य समझता था। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर जो प्रमाण-पत्र मिलते हैं उनके कागज का मूल्य एक-दो पैसे ही होगा पर वह कागज कितना मूल्यवान है- इसको वह परीक्षोत्तीर्ण छात्र ही जानता है। सरकारी कर्मचारियों के पद की पहचान के लिए धातु के बने अक्षर मिलते हैं, जो कि कन्धे या कपड़ों में लगा दिये जाते हैं। यह कर्मचारी जानते हैं कि उन्हें लगा लेने पर और उतार देने पर उनको जनता कितने अन्तर से पहचानती है। यज्ञोपवीत भी एक ऐसा ही प्रतीक है, जो बाजारू कीमत से भले ही कम हो; पर उसके पीछे एक महान् तत्त्वज्ञान जुड़ा हुआ है। इसलिये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जनेऊ पहनना कन्धे पर एक डोरा लटका लेना है, वरन् इस प्रकार सोचना चाहिए कि मनुष्य की दैवी जिम्मेदारियों का एक प्रतीक हमारे कन्धे पर अवस्थित है।
यह पूछा जाता है कि मन में कोई बात हो, तो उसी से सब कुछ हो सकता है, इसके लिये वाह्य-चिह्न धारण करने की क्या आवश्यकता है ? जब मन में द्विजत्व ग्रहण करने के भाव मौजूद हों, तो उसका होना ही पर्याप्त है। फिर यज्ञोपवीत क्यों पहनें ? और यदि मन में उस प्रकार की भावना नहीं है, तो जनेऊ पहनने से भी कुछ लाभ नहीं।
मोटे तौर से तर्क ठीक प्रतीत होता है, परन्तु जिन्होंने मनुष्य की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि इस तर्क में कितना कम तथ्य है। बुराई की ओर, अधर्म की ओर, पाशविक भोगों की ओर, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस ओर मन अपने आप चलता है, पर उसे त्याग के, संयम के, धर्म के मार्ग पर चलने के लिये बड़े-बड़े कष्ट साध्य प्रयत्न करने पड़ते हैं। पानी को बहाया जाय, तो वह जिधर नीची भूमि होगी, वह बिना किसी प्रयत्न के अपने आप अपना रास्ता बनाता हुआ बहेगा। निचाई जितना अधिक होगी, उतना ही पानी का बहाव तेज होता जायेगा, परन्तु यदि पानी को ऊपर चढ़ाना है, तो यह कार्य अपने आप नहीं हो सकता, इसके लिये तरह-तरह के साधन जुटाने पड़ेंगे। नल, पम्प, टंकी, आदि का कोई माध्यम लगाकर उसके पीछे ऐसी शक्ति का संयोग करना पड़ता है, जिसके दबाव से पानी ऊपर चढ़े। दबाव वाली शक्ति तथा पानी को ऊपर ले जाने वाले साधन यदि अच्छे हुए तो, वह तेजी से और अधिक मात्रा में ऊपर चढ़ता है, यदि वह साधन निर्बल हुए तो पानी चढ़ने की गति मन्द हो जायेगी।
यही बात जीव को उच्च मार्ग में लगाने के संबंध में भी है। यदि धर्म-मार्ग में, सिद्धान्तमय उच्चपथ में प्रगति करनी है, तो उसके लिए ऐसे प्रयत्न करने पड़ते हैं, जैसे कि पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए करने पड़ते हैं। सोलह संस्कार, नाना प्रकार के धार्मिक कर्म-काण्ड, व्रत, जप, पूजा, अनुष्ठान, तीर्थयात्रा, दान-पुण्य, स्वाध्याय, सत्संग ऐसे ही प्रयोजन हैं, जिसके द्वारा मन को प्रभावित, अभ्यस्त और संस्कृत बनाकर दिव्यत्व की ओर- द्विजत्व की ओर- बढ़ाया जाता है। इन सबका उद्देश्य मात्र केवल इतना ही है कि मन पाशविक वृत्तियों से मुड़कर दिव्यत्व की ओर अग्रसर हो, यदि ऐसा करना अपने आप ही सरलतापूर्वक हुआ तो यज्ञोपवीत को व्यर्थ बताने वाले तक को स्वीकार करने में किसी को कुछ आपत्ति न होगी। उस दिशा में यह पृथ्वी ब्रह्मलोक होती और वैसा समय सतयुग कहा जाता। पर आज तो वैसा नहीं है। हमारे मनों की कुटिलता इतनी बढ़ी हुई है कि आध्यात्मिक साधना करने वाले भी बार-बार भ्रष्ट हो जाते हैं, तब ऐसी आशा रखना कहा तक उचित है कि अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जायेगा।
यज्ञोपवीत धारण करना इसलिए आवश्यक है कि इससे एक प्रेरणा नियमित रूप से मिलती है। जिनके जिम्मे संसार के बड़े-बड़े कार्य हैं, जिनका जीवन व्यवस्थित है, वे सबेरे ही अपना कार्यक्रम बनाकर मेज के सामने लटका लेते हैं और उस तख्ती पर बार-बार निगाह डालकर अपने कार्यक्रम को यथोचित बनाते रहते हैं। यदि वह याद दिलाने वाली तख्ती न हो, तो उनके कार्यक्रम में गड़बड़ पड़ सकती है। यद्यपि उस तख्ती का स्वतः कोई बड़ा मूल्य नहीं है, पर उसके आधार पर काम करने वाले का अमूल्य समय व्यवस्थित रहता है। इसलिए उसका लाभ असाधारण महत्त्वपूर्ण है और उस महान् लाभ का श्रेय उस तख्ती को कम नहीं है। जनेऊ ऐसी ही एक तख्ती है, जो हमारे जीवनोद्देश्य और जीवन-क्रम को व्यवस्थित रखने की याद हर घड़ी दिलाती रहती है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book