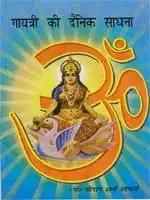|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> गायत्री की दैनिक साधना गायत्री की दैनिक साधनाश्रीराम शर्मा आचार्य
|
151 पाठक हैं |
||||||
गायत्री की दैनिक साधना
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
दैनिक गायत्री उपासना
गायत्री उपासना प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म-कृत्य है। वैसे द्विज,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कहते हैं। जो लोग यज्ञोपवीत धारण कर सकते
हैं, वे द्विज हैं। ऐसे सभी लोगों को गायत्री का अधिकार है। द्विज वह है,
जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। एक जन्म माता-पिता के राज-वीर्य से सभी का होता
है, इसलिए मनुष्य और पशु सभी समान हैं। दूसरा आध्यात्मिक जन्म गायत्री
माता और यज्ञ पिता के संयोग से होता है। गायत्री अर्थात् सद्बुद्धिरूपिणी
माता और यज्ञ अर्थात् परमार्थरूपी पिता को जिन्होंने अपना आध्यात्मिक
माता-पिता समझ लिया है, जीवन की वस्तु समझकर परमार्थ एवं आत्म-कल्याण का
साधन स्वीकार किया है, वस्तुत: वे द्विज हैं। गायत्री उपासक इसी श्रेणी के
होते हैं। जो गायत्री उपासना में लगे रहते हैं, वे ऐसे हो जाते हैं। इसी
प्रकार गायत्री और द्विजत्व एक साथ रहते हैं। इसी एकता के अभाव को संस्कृत
में अनधिकार कहा है। जिनमें इस प्रकार की एकता न हो, वे अनधिकारी कहे जाते
हैं। उच्च भावना और गायत्री से संबंध बनाये रखने के लिए अधिकारी की
प्रतिष्ठा की गई है।
यज्ञापवीत को गायत्री की मूर्ति-प्रतिमा कहना चाहिए। गायत्री को हर घड़ी छाती से लगाए रखना, हृदय पर धारण किए रहना यज्ञोपवीत का उद्देश्य है। जनेऊ में तीन तार होते हैं-गायत्री में तीन चरण हैं। उपवीत में नौ लड़ें हैं, गायत्री में नौ शब्द है। यज्ञोपवीत में तीन मध्य ग्रंथियाँ और एक ब्रह्म-ग्रंथि होती है-गायत्री में तीन व्याहृतियाँ और एक प्रणव है। अन्य देवताओं की मूर्तियाँ पत्थर, धातु आदि की बनाई जाती हैं, पर उनका पूजन और ध्यान तो उपासना-गृह में ही हो सकता है, किन्तु गायत्री देवता तो मनुष्य का जीवन प्राण ही है, उसका पूजन किसी नियत समय पर किसी नियत स्थान पर कर देने से काम नहीं चल सकता। वह देवता तो ऐसा है जिसको सोते-जागते, चलते-फिरते, खाते-नहाते हर समय साथ रखना है। इसलिए उसकी प्रतिमा धातु या पत्थर की न बनाकर सूत की बनाई गई। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमयी प्रतिमा है। इसको प्राणप्रिय समझकर हर घड़ी छाती पर, कंधे पर धारण किए रहने के लिए यज्ञोपवीत पहना जाता है। गायत्री उपासक के लिए यज्ञोपवीत धारण करना एक उचित कर्त्तव्य है।
अपनी बुद्धि को सात्त्विक, सन्मार्गगामी बनाने के लिए पूरी तत्परता से कार्य करना यही यज्ञोपवीत धारण करने का लक्ष्य है। यज्ञोपवीत को सूत्र भी कहते हैं, सूत्र डोरे को भी कहते हैं, उस शब्द रचना को भी कहते हैं जो स्वयं बहुत संक्षिप्त होते हुए भी अपने अंदर एक विस्तृत अर्थ छिपाए होती है। अष्टाध्यायी, षट्दर्शन, गृहसूत्र आदि ऐसे ही ग्रंथ हैं। यज्ञोपवीत में लिपि और भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है तो भी वह ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है। इन शिक्षाओं को हर घड़ी ध्यान रखने के लिए ही यज्ञोपवीत पहना जाता है और उसे पहनने पर इतना जोर दिया जाता है।
गायत्री को गुरुमंत्र कहा जाता है। प्राचीनकाल में बालक जब गुरुकुल में विद्या पढ़ने जाते थे, तो उन्हें वेदारंभ संस्कार के समय गुरुमंत्र के रूप में गायत्री मंत्र की ही शिक्षा दी जाती थी। वेद आरंभ वेदमाता गायत्री से ही होता है। आज के नामधारी गुरु नाना प्रकार के ऊट-पटाँग मंत्र पढ़कर गुरु दीक्षा की लकीर पीटते हैं, पर प्राचीनकाल में गायत्री मंत्र के अतिरिक्त और कोई दीक्षा मंत्र न था। भारतीय धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक तीन जीवित देवता भी माने गए हैं। (1) माता, (2) पिता, (3) गुरु। जिस प्रकार व्यक्ति के माता-पिता होना आवश्यक है, उसी प्रकार उसका गुरु होना भी आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपनी माता का पता न बता सके या अपने पिता के संबंध में अपरिचित रहे, तो उसकी उत्पत्ति अनैतिक मानी जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गुरु रहित हो तो उसको भी असंस्कृत कहा जाएगा। निगुरा एक प्रकार की गाली है। जिसका गुरु नहीं, उसकी आध्यात्मिक सुव्यवस्था संदिग्ध मानी जाती है। गायत्री दीक्षा या गुरु दीक्षा एक ही बात है।
ऐसा उल्लेख मिलता है कि गायत्री मंत्र कीलित है। इसको वशिष्ठ तथा विश्वामित्र ऋषियों का शाप लगा हुआ है। जो उस शाप का उत्कीलन कर लेता है, उसी की साधना सफल होती है। इस अलंकारिक वर्णन में विधिवत गायत्री साधना करने, उसकी शास्त्रीय प्रक्रिया को समझने एवं अनुभवी पथ प्रदर्शक के ही संरक्षण में साधना क्रम को आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया है। वशिष्ठ कहते हैं-विशेष रूप से श्रेष्ठ को। प्राचीन काल में जो व्यक्ति सवा करोड़ गायत्री जब कर लेते थे, उन्हें वशिष्ठ की पदवी दी जाती थी, रघुवंशियों के कुल गुरु सदा ऐसे ही, वशिष्ठ पदवीधारी होते थे। रघु, अज, दिलीप, दशरथ, राम, लव, कुश, उन छह पीढ़ियों के गुरु एक वशिष्ठ नहीं अलग-अलग ऋषि थे, पर उन सभी ने उपासना के आधार पर वशिष्ठ पद पाया था। वशिष्ठ शाप मोचन का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के किसी अनुभवी उपासक से गायत्री साधना की शिक्षा लेनी चाहिए, उसे अपना पथ प्रदर्शक नियुक्त करना चाहिए। विश्वामित्र का अर्थ-संसार की भलाई करने वाले परमार्थी सच्चरित्र एवं कर्त्तव्यनिष्ठ। गायत्री का शिक्षक केवल वसिष्ठ गुण वाला ही होना पर्याप्त नहीं, उसे विश्वामित्र भी होना चाहिए। तपस्वी और परमार्थी दोनों गुण जिसमें हो उन्हें वशिष्ठ एवं विश्वामित्र की श्रेणी का व्यक्ति कहा जा सकता। ऐसे ही लोगों से गायत्री की विधिवत शिक्षा-दीक्षा लेने पर महामंत्र से वह लाभ उठाना संभव होता है। अपने आप मन चाहे तरीकों से कुछ-न-कुछ करने लगने से अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जिसने उपयुक्त पथ प्रदर्शक प्राप्त कर लिया, उसने साधना की आधी मंजिल पार कर ली ऐसा समझ लेना चाहिए। यही शाप मोचन और उत्कीलन है। गायत्री जैसी विश्व जननी महाशक्ति को कोई भी सत्ता शाप देने में समर्थ नहीं हो सकती। गुरु की महत्ता को प्रतिपादन करने के लिए कहीं अलंकारिक रूप में शाप लगने की बात कही गयी है।
यज्ञोपवीत धारण करना, गुरु दीक्षा लेना, विधिवत् मंत्र ग्रहण करना ये तीनों बातें गायत्री उपासना में सहायक, लाभदायक, आवश्यक एवं मंजिल को पार करने में बड़ी सरलता उत्पन्न कर देने वाली हैं, फिर भी अनिवार्य नहीं कि इन बातों के बिना साधना नहीं हो सकती हो या गायत्री उपासना न की जा सकती हो, सो बात नहीं है। ईश्वर की वाणी, वेद ऋचा, भगवती महाशक्ति गायत्री को अपनाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। शास्त्र विधान के अनुसार ब्राह्मण बालक का 12 वर्ष, क्षत्रिय का 14 वर्ष, वैश्य का 20 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत होना चाहिए। इससे अधिक आयु हो जाने पर जल्दी की दृष्टि से बिना किसी विशेष समारोह के किसी भी यज्ञ आदि के शुभ अवसर पर साधारण रीति से यज्ञोपवीत धारण किया जा सकता है, पर जिनको ऐसी सुविधा भी न हो, उन्हें यज्ञोपवीत के लिए गायत्री उपासना रोकने की आवश्यकता नहीं है। अवसर आने पर वे पीछे भी जनेऊ ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि अपने स्थान पर ठीक पथ-प्रदर्शक गुरु प्राप्त न हो, तो किसी दूरस्थ व्यक्ति से संपर्क स्थापित करके भी काम चलाया जा सकता है।
पुरुषों की भाँति स्त्रियाँ भी गायत्री उपासना से लाभान्वित हो सकती हैं। कई आध्यात्मिक तत्त्ववेत्ताओं का यह कहना है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को गायत्री उपासना का लाभ अधिक मिलता है, क्योंकि माताओं को स्वभावत: पुत्र की अपेक्षा कन्या का अधिक ध्यान रहता है। वह अपनी पुत्रियों के लिए अधिक उदारता का परिचय देती हैं।
विधिपूर्वक साधना एक महत्त्वपूर्ण बात है। किसी कार्य को उचित क्रिया पद्धति के साथ किया जाय, तो उसका लाभ और फल ठीक प्रकार का होता है। अविधिपूर्वक किए हुए कार्य तो असफल रहते हैं या उनका स्वल्प फल होता है। इसलिए गायत्री उपासकों का विधि-विधान भली प्रकार समझ लेना चाहिए।
शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणत: स्नान द्वारा ही शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में हाथ-मुँह धोकर गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। साधना के समय जिन सूती वस्त्रों को शरीर पर धारण किया जाय, वह धुले होने चाहिए। पालथी मारकर सीधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्टसाध्य आसनों से चित्त में अस्थिरता आती है। बिना बिछाए जमीन पर न बैठना चाहिए। कुश का आसन, चटाई आदि के आसन सर्वोत्तम हैं। पशु-चर्म गायत्री साधना के उपयुक्त नहीं।
यज्ञापवीत को गायत्री की मूर्ति-प्रतिमा कहना चाहिए। गायत्री को हर घड़ी छाती से लगाए रखना, हृदय पर धारण किए रहना यज्ञोपवीत का उद्देश्य है। जनेऊ में तीन तार होते हैं-गायत्री में तीन चरण हैं। उपवीत में नौ लड़ें हैं, गायत्री में नौ शब्द है। यज्ञोपवीत में तीन मध्य ग्रंथियाँ और एक ब्रह्म-ग्रंथि होती है-गायत्री में तीन व्याहृतियाँ और एक प्रणव है। अन्य देवताओं की मूर्तियाँ पत्थर, धातु आदि की बनाई जाती हैं, पर उनका पूजन और ध्यान तो उपासना-गृह में ही हो सकता है, किन्तु गायत्री देवता तो मनुष्य का जीवन प्राण ही है, उसका पूजन किसी नियत समय पर किसी नियत स्थान पर कर देने से काम नहीं चल सकता। वह देवता तो ऐसा है जिसको सोते-जागते, चलते-फिरते, खाते-नहाते हर समय साथ रखना है। इसलिए उसकी प्रतिमा धातु या पत्थर की न बनाकर सूत की बनाई गई। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमयी प्रतिमा है। इसको प्राणप्रिय समझकर हर घड़ी छाती पर, कंधे पर धारण किए रहने के लिए यज्ञोपवीत पहना जाता है। गायत्री उपासक के लिए यज्ञोपवीत धारण करना एक उचित कर्त्तव्य है।
अपनी बुद्धि को सात्त्विक, सन्मार्गगामी बनाने के लिए पूरी तत्परता से कार्य करना यही यज्ञोपवीत धारण करने का लक्ष्य है। यज्ञोपवीत को सूत्र भी कहते हैं, सूत्र डोरे को भी कहते हैं, उस शब्द रचना को भी कहते हैं जो स्वयं बहुत संक्षिप्त होते हुए भी अपने अंदर एक विस्तृत अर्थ छिपाए होती है। अष्टाध्यायी, षट्दर्शन, गृहसूत्र आदि ऐसे ही ग्रंथ हैं। यज्ञोपवीत में लिपि और भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है तो भी वह ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है। इन शिक्षाओं को हर घड़ी ध्यान रखने के लिए ही यज्ञोपवीत पहना जाता है और उसे पहनने पर इतना जोर दिया जाता है।
गायत्री को गुरुमंत्र कहा जाता है। प्राचीनकाल में बालक जब गुरुकुल में विद्या पढ़ने जाते थे, तो उन्हें वेदारंभ संस्कार के समय गुरुमंत्र के रूप में गायत्री मंत्र की ही शिक्षा दी जाती थी। वेद आरंभ वेदमाता गायत्री से ही होता है। आज के नामधारी गुरु नाना प्रकार के ऊट-पटाँग मंत्र पढ़कर गुरु दीक्षा की लकीर पीटते हैं, पर प्राचीनकाल में गायत्री मंत्र के अतिरिक्त और कोई दीक्षा मंत्र न था। भारतीय धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक तीन जीवित देवता भी माने गए हैं। (1) माता, (2) पिता, (3) गुरु। जिस प्रकार व्यक्ति के माता-पिता होना आवश्यक है, उसी प्रकार उसका गुरु होना भी आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपनी माता का पता न बता सके या अपने पिता के संबंध में अपरिचित रहे, तो उसकी उत्पत्ति अनैतिक मानी जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गुरु रहित हो तो उसको भी असंस्कृत कहा जाएगा। निगुरा एक प्रकार की गाली है। जिसका गुरु नहीं, उसकी आध्यात्मिक सुव्यवस्था संदिग्ध मानी जाती है। गायत्री दीक्षा या गुरु दीक्षा एक ही बात है।
ऐसा उल्लेख मिलता है कि गायत्री मंत्र कीलित है। इसको वशिष्ठ तथा विश्वामित्र ऋषियों का शाप लगा हुआ है। जो उस शाप का उत्कीलन कर लेता है, उसी की साधना सफल होती है। इस अलंकारिक वर्णन में विधिवत गायत्री साधना करने, उसकी शास्त्रीय प्रक्रिया को समझने एवं अनुभवी पथ प्रदर्शक के ही संरक्षण में साधना क्रम को आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया है। वशिष्ठ कहते हैं-विशेष रूप से श्रेष्ठ को। प्राचीन काल में जो व्यक्ति सवा करोड़ गायत्री जब कर लेते थे, उन्हें वशिष्ठ की पदवी दी जाती थी, रघुवंशियों के कुल गुरु सदा ऐसे ही, वशिष्ठ पदवीधारी होते थे। रघु, अज, दिलीप, दशरथ, राम, लव, कुश, उन छह पीढ़ियों के गुरु एक वशिष्ठ नहीं अलग-अलग ऋषि थे, पर उन सभी ने उपासना के आधार पर वशिष्ठ पद पाया था। वशिष्ठ शाप मोचन का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के किसी अनुभवी उपासक से गायत्री साधना की शिक्षा लेनी चाहिए, उसे अपना पथ प्रदर्शक नियुक्त करना चाहिए। विश्वामित्र का अर्थ-संसार की भलाई करने वाले परमार्थी सच्चरित्र एवं कर्त्तव्यनिष्ठ। गायत्री का शिक्षक केवल वसिष्ठ गुण वाला ही होना पर्याप्त नहीं, उसे विश्वामित्र भी होना चाहिए। तपस्वी और परमार्थी दोनों गुण जिसमें हो उन्हें वशिष्ठ एवं विश्वामित्र की श्रेणी का व्यक्ति कहा जा सकता। ऐसे ही लोगों से गायत्री की विधिवत शिक्षा-दीक्षा लेने पर महामंत्र से वह लाभ उठाना संभव होता है। अपने आप मन चाहे तरीकों से कुछ-न-कुछ करने लगने से अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जिसने उपयुक्त पथ प्रदर्शक प्राप्त कर लिया, उसने साधना की आधी मंजिल पार कर ली ऐसा समझ लेना चाहिए। यही शाप मोचन और उत्कीलन है। गायत्री जैसी विश्व जननी महाशक्ति को कोई भी सत्ता शाप देने में समर्थ नहीं हो सकती। गुरु की महत्ता को प्रतिपादन करने के लिए कहीं अलंकारिक रूप में शाप लगने की बात कही गयी है।
यज्ञोपवीत धारण करना, गुरु दीक्षा लेना, विधिवत् मंत्र ग्रहण करना ये तीनों बातें गायत्री उपासना में सहायक, लाभदायक, आवश्यक एवं मंजिल को पार करने में बड़ी सरलता उत्पन्न कर देने वाली हैं, फिर भी अनिवार्य नहीं कि इन बातों के बिना साधना नहीं हो सकती हो या गायत्री उपासना न की जा सकती हो, सो बात नहीं है। ईश्वर की वाणी, वेद ऋचा, भगवती महाशक्ति गायत्री को अपनाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। शास्त्र विधान के अनुसार ब्राह्मण बालक का 12 वर्ष, क्षत्रिय का 14 वर्ष, वैश्य का 20 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत होना चाहिए। इससे अधिक आयु हो जाने पर जल्दी की दृष्टि से बिना किसी विशेष समारोह के किसी भी यज्ञ आदि के शुभ अवसर पर साधारण रीति से यज्ञोपवीत धारण किया जा सकता है, पर जिनको ऐसी सुविधा भी न हो, उन्हें यज्ञोपवीत के लिए गायत्री उपासना रोकने की आवश्यकता नहीं है। अवसर आने पर वे पीछे भी जनेऊ ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि अपने स्थान पर ठीक पथ-प्रदर्शक गुरु प्राप्त न हो, तो किसी दूरस्थ व्यक्ति से संपर्क स्थापित करके भी काम चलाया जा सकता है।
पुरुषों की भाँति स्त्रियाँ भी गायत्री उपासना से लाभान्वित हो सकती हैं। कई आध्यात्मिक तत्त्ववेत्ताओं का यह कहना है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को गायत्री उपासना का लाभ अधिक मिलता है, क्योंकि माताओं को स्वभावत: पुत्र की अपेक्षा कन्या का अधिक ध्यान रहता है। वह अपनी पुत्रियों के लिए अधिक उदारता का परिचय देती हैं।
विधिपूर्वक साधना एक महत्त्वपूर्ण बात है। किसी कार्य को उचित क्रिया पद्धति के साथ किया जाय, तो उसका लाभ और फल ठीक प्रकार का होता है। अविधिपूर्वक किए हुए कार्य तो असफल रहते हैं या उनका स्वल्प फल होता है। इसलिए गायत्री उपासकों का विधि-विधान भली प्रकार समझ लेना चाहिए।
शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणत: स्नान द्वारा ही शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में हाथ-मुँह धोकर गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। साधना के समय जिन सूती वस्त्रों को शरीर पर धारण किया जाय, वह धुले होने चाहिए। पालथी मारकर सीधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्टसाध्य आसनों से चित्त में अस्थिरता आती है। बिना बिछाए जमीन पर न बैठना चाहिए। कुश का आसन, चटाई आदि के आसन सर्वोत्तम हैं। पशु-चर्म गायत्री साधना के उपयुक्त नहीं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book