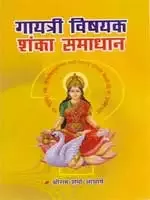|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> गायत्री विषयक शंका समाधान गायत्री विषयक शंका समाधानश्रीराम शर्मा आचार्य
|
277 पाठक हैं |
||||||
गायत्री विषयक शंका समाधान
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
गायत्री एक या अनेक
गायत्री महामंत्र एक है। वेदमाता भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री,
आद्यशक्ति के नाम से प्रख्यात गायत्री एक ही है। वहीं संध्यावंदन में
प्रयुक्त होती है। यज्ञोपवीत संस्कार के समय गुरूदीक्षा के रूप में भी उसी
को दिया जाता है। इसलिए उसे गुरु मंत्र भी कहते है। अनुष्ठान-पुरश्चरण इसी
आद्यशक्ति के होते है या ब्रह्मविद्या है ऋतुम्भरा प्रज्ञा है। सामान्य
नित्य उपासना से लेकर विशिष्टतम साधनाएं इसी प्रख्यात गायत्री मंत्र के
माध्यम से होती है। इसके स्थान पर या सामान्तर किसी और गायत्री को
प्रतिद्वन्द्वी के रूप में खड़ा नहीं किया जा सकता। मध्यकालीन अराजकता के
अन्धकार भरे अराजकता भर दिनों में उपासना विज्ञान की उठक-पटक खूब हुई और
स्वेच्छाचार फैलाने में निरंकुशता बरती गई। उन्हीं दिनों ब्राह्मण
क्षत्रिय वैश्य वर्ग की अलग-अलग गायत्री गढ़ी गई उन्हीं दिनों
देवी-देवताओं के नाम से अलग-अलग गायत्रियों का सृजन हुआ।
गायत्री महामंत्र की प्रमुखता और मान्यता का लाभ उठाने के लिए देववादियों ने अपने प्रिय देवता के नाम पर गायत्री बनाई और फैलाई होगी। उन्हीं का संग्रह करके किसी ने चौबीस देव गायत्री बना दी प्रतीत होती है। देव मन्त्र यदि गायत्री छन्द में बने हो तो हर्ज ही नहीं पर उसमें से किसी के भी महामंत्र को गायत्री का प्रतिद्वंदी या स्थानापन्न नहीं बनाना चाहिए। और न जाति वंश के नाम पर उपासना क्षेत्र में फूट-फसाद खड़ा करना चाहिए। देवलोक में कामधेनु एक ही है। और धरती पर भी गंगा की तरह गायत्री भी एक ही है। चौबीस अक्षर आठ-आठ अक्षरों के तीन चरण –तीन व्याह्यतियाँ -एक ओंकार इतना ही आद्य गायत्री का स्वरूप है। उसी जो जाति, लिंग आदि का भेद किए बिना सर्वजनीन- सार्वभौम उपासना के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए।
गायत्री के चौबीस अक्षरों में से प्रत्येक में से एक-एक प्रेरणा और सामर्थ्य छिपी पड़ी है। उसे ध्यान में रखते हुए चौबीस महा-मातृकाओं का उल्लेख है या तो एक दूसरे की प्रतिद्वन्दी है और आद्यशक्ति की समग्र क्षमता के स्थानापन्न होने के उपयुक्त है और हर अक्षर का तत्वदर्शन एवं साधना क्षेत्र निरूपित करने के लिए चौबीस प्रतिमाओं का स्वरूप निर्धारित हुआ है यह एक ही तत्व के भेद एक-एक करके समझाने और एक-एक चरण में दिव्य सामर्थों का रहस्य, उद्घाटन करने की प्रक्रिया भी है।
नवदुर्गाओं की तरह गायत्री महाशक्ति के भी नौ विभाग है, उन्हें नव देवियाँ कहते है। इस विभाजन को अध्याय-प्रकरण के तुल्य माना जा सकता है। महामन्त्र के तीन चरणों में से प्रत्येक में तीन-तीन शब्द है। इस तरह यह शब्द परिवार सौर -परिवार के नौ शब्दों की तरह बन जाता है। यज्ञोपवीत के नौ विभाजन वर्गीकरण के संकेत देते और विवेचना की सुविधा प्रस्तुत करते है। इस आधार पर गायत्री -तत्त्व मण्डल में नौ देवियों को मान्यता मिली और इसकी पृथक-पृथक प्रतिमा बनाई गई है।
ब्रह्मतत्व व्यापक एवं निराकार है, पर उनकी विभिन्न सामर्थ्यों की विवेचना करने की दृष्टि से देवताओं का स्वरुप एवं प्रयोजन निर्धारत किया गया है। गायत्री के नौ शब्दों की नौ देवियाँ चौबीस अक्षरों की चौबीस मातृकाओं की प्रतिमाएं बनी हैं। यह एक ही महाशक्ति -सागर की छोटी- बड़ी लहरें है। इस भिन्नता में भी एकता का दर्शन है-अंग -अवयवों को मिलाकर काया बनती है। आद्यशक्ति की प्रेरणाओं, शिक्षिका, सामर्थ्यो, सिद्धियों का निरूपण ही इन प्रतीक प्रतिमाओं के अन्तर्गत हुआ है। अतएव गायत्री एक ही है प्रतिमाओ में भिन्नता होते हुए भी उसकी तात्विक एकता में अन्तर नहीं आता।
गायत्री एक मुखी सावित्री पंचमुखी है। गायत्री आत्मिकी और सावित्री भौतिकी है। एक को ऋद्धि और दूसरी को सिद्धि कहते है। रुपये के दोनों ओर दो आकृतियाँ होती है, पर इससे रुपया दो नहीं हो जाता। गायत्री और सावित्री दोनों एक ही तथ्य की दो प्रतिक्रियाएं है जैसे आग में गर्मी और रोशनी दो वस्तुएँ होती हैं, उसी प्रकार गायत्री सावित्री के युग्म को परस्पर अविच्छिन्न समझना चाहिए।
त्रिकाल संध्या में ब्राह्मी-वैष्णवी-शांभवी की तीन आकृतियों की प्रतिष्ठापना की जाती है अन्याय प्रयोजनों के लिए उनकी अन्य आकृतियाँ ध्यान एवं पूजन के लिए प्रयुक्त होती हैं। यह कलेवर भिन्नता ऐसी ही है जैसे एक ही व्यक्ति सैनिक मिश्री, खिलाड़ी, तैराक, नट, दूल्हा आदि बनने के समय भिन्न-भिन्न बाह्य उपकरणों को धारण किये होता है, भिन्न मुद्राओं में देखा जाता है उसी प्रकार एक ही महाशक्ति विभिन्न कार्यो में रहते समय विभिन्न स्वरूपों में दृष्टिगोचर होती है। यही बात गायत्री माता को विभिन्न आकृतियों के सम्बध में समझी जानी चाहिए।
गायत्री महामंत्र की प्रमुखता और मान्यता का लाभ उठाने के लिए देववादियों ने अपने प्रिय देवता के नाम पर गायत्री बनाई और फैलाई होगी। उन्हीं का संग्रह करके किसी ने चौबीस देव गायत्री बना दी प्रतीत होती है। देव मन्त्र यदि गायत्री छन्द में बने हो तो हर्ज ही नहीं पर उसमें से किसी के भी महामंत्र को गायत्री का प्रतिद्वंदी या स्थानापन्न नहीं बनाना चाहिए। और न जाति वंश के नाम पर उपासना क्षेत्र में फूट-फसाद खड़ा करना चाहिए। देवलोक में कामधेनु एक ही है। और धरती पर भी गंगा की तरह गायत्री भी एक ही है। चौबीस अक्षर आठ-आठ अक्षरों के तीन चरण –तीन व्याह्यतियाँ -एक ओंकार इतना ही आद्य गायत्री का स्वरूप है। उसी जो जाति, लिंग आदि का भेद किए बिना सर्वजनीन- सार्वभौम उपासना के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए।
गायत्री के चौबीस अक्षरों में से प्रत्येक में से एक-एक प्रेरणा और सामर्थ्य छिपी पड़ी है। उसे ध्यान में रखते हुए चौबीस महा-मातृकाओं का उल्लेख है या तो एक दूसरे की प्रतिद्वन्दी है और आद्यशक्ति की समग्र क्षमता के स्थानापन्न होने के उपयुक्त है और हर अक्षर का तत्वदर्शन एवं साधना क्षेत्र निरूपित करने के लिए चौबीस प्रतिमाओं का स्वरूप निर्धारित हुआ है यह एक ही तत्व के भेद एक-एक करके समझाने और एक-एक चरण में दिव्य सामर्थों का रहस्य, उद्घाटन करने की प्रक्रिया भी है।
नवदुर्गाओं की तरह गायत्री महाशक्ति के भी नौ विभाग है, उन्हें नव देवियाँ कहते है। इस विभाजन को अध्याय-प्रकरण के तुल्य माना जा सकता है। महामन्त्र के तीन चरणों में से प्रत्येक में तीन-तीन शब्द है। इस तरह यह शब्द परिवार सौर -परिवार के नौ शब्दों की तरह बन जाता है। यज्ञोपवीत के नौ विभाजन वर्गीकरण के संकेत देते और विवेचना की सुविधा प्रस्तुत करते है। इस आधार पर गायत्री -तत्त्व मण्डल में नौ देवियों को मान्यता मिली और इसकी पृथक-पृथक प्रतिमा बनाई गई है।
ब्रह्मतत्व व्यापक एवं निराकार है, पर उनकी विभिन्न सामर्थ्यों की विवेचना करने की दृष्टि से देवताओं का स्वरुप एवं प्रयोजन निर्धारत किया गया है। गायत्री के नौ शब्दों की नौ देवियाँ चौबीस अक्षरों की चौबीस मातृकाओं की प्रतिमाएं बनी हैं। यह एक ही महाशक्ति -सागर की छोटी- बड़ी लहरें है। इस भिन्नता में भी एकता का दर्शन है-अंग -अवयवों को मिलाकर काया बनती है। आद्यशक्ति की प्रेरणाओं, शिक्षिका, सामर्थ्यो, सिद्धियों का निरूपण ही इन प्रतीक प्रतिमाओं के अन्तर्गत हुआ है। अतएव गायत्री एक ही है प्रतिमाओ में भिन्नता होते हुए भी उसकी तात्विक एकता में अन्तर नहीं आता।
गायत्री एक मुखी सावित्री पंचमुखी है। गायत्री आत्मिकी और सावित्री भौतिकी है। एक को ऋद्धि और दूसरी को सिद्धि कहते है। रुपये के दोनों ओर दो आकृतियाँ होती है, पर इससे रुपया दो नहीं हो जाता। गायत्री और सावित्री दोनों एक ही तथ्य की दो प्रतिक्रियाएं है जैसे आग में गर्मी और रोशनी दो वस्तुएँ होती हैं, उसी प्रकार गायत्री सावित्री के युग्म को परस्पर अविच्छिन्न समझना चाहिए।
त्रिकाल संध्या में ब्राह्मी-वैष्णवी-शांभवी की तीन आकृतियों की प्रतिष्ठापना की जाती है अन्याय प्रयोजनों के लिए उनकी अन्य आकृतियाँ ध्यान एवं पूजन के लिए प्रयुक्त होती हैं। यह कलेवर भिन्नता ऐसी ही है जैसे एक ही व्यक्ति सैनिक मिश्री, खिलाड़ी, तैराक, नट, दूल्हा आदि बनने के समय भिन्न-भिन्न बाह्य उपकरणों को धारण किये होता है, भिन्न मुद्राओं में देखा जाता है उसी प्रकार एक ही महाशक्ति विभिन्न कार्यो में रहते समय विभिन्न स्वरूपों में दृष्टिगोचर होती है। यही बात गायत्री माता को विभिन्न आकृतियों के सम्बध में समझी जानी चाहिए।
स्नान और उनकी अनिवार्यता
गायत्री जप बिना स्नान किए भी हो सकता है या नहीं ? इस प्रश्न के उत्तर
में समझा जाना चाहिए कि प्रत्येक अध्यात्म प्रयोजन के लिए शास्त्रों में
शरीर को स्नान से शुद्ध करके और धुले हुए कपड़े पहनकर बैठने का विधान है।
अधिक कपड़े पहनने पर सभी कपड़े नित्य धुले हुए हों, यह व्यवस्था करना कठिन
पड़ता है। इसलिए धोती दुपट्टा पहनकर बैठने की परम्परा है। ठण्ड लगती हो तो
बनियान आदि पहन सकते हैं, पर वे भी धुले ही होने चाहिए। यह पूर्ण विधान
हुआ।
अब कठिनाईवश इस व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि शास्त्रकारों ने कठिनाई की स्थिति में लचीली नीति रखी है। ऐसे कड़े प्रतिबन्ध नहीं लगाएं जिनके कारण स्नान एवं धुले वस्त्र की व्यवस्था न बन पड़ने पर जप जैसा पुनीत कार्य भी बन्द कर दिया जाय। उसमें तो दुहरी हानि हुई। नियम इसलिए बने थे कि उपासना काल में अधिकतम पवित्रता रखने का प्रयत्न किया जाए। यदि नियम इतना कड़ा हो जाय कि स्नानदि न बन पड़ने पर जप, साधना का उपार्जन ही बन्द हो जाय तब बात उल्टी हो गई। नियमों की कड़ाई ने ही साधना, उपासना कृत्य से वंचित करके, कठिनाई का हल निकालने के स्थान पर रही बची संभावना भी समाप्त कर दी। जो आधा-अधूरा लाभ मिल सकता था उसकी सम्भावना भी समाप्त हो गई।
शास्त्र-विधान यह है कि शरीर, वस्त्र, पात्र, उपासना, पूजा, सामग्री, देव प्रतिमा, आसन, स्नान आदि सभी को अधिकतम स्वच्छ बनाकर उपासना कृत्य करने पर जोर दिया जाए। इसमें आलस्य-प्रमाद को हटाने और स्वच्छता को उपासना का अंग मानने की बात कही गई है। फिर भी कारणवश ऐसी कठिनाइयाँ हो सकती है, जिसमें साधक की मन-स्थिति और परिस्थिति पर ध्यान देते हुए विधान-प्रक्रिया को उस सीमा तक ढीला किया जाय, जितना किए बिना गाड़ी रुक जाने का खतरा हो। स्वच्छता की नीति पूरी तरह तो समाप्त नहीं करनी चाहिए, पर जहां तक अधिकाधिक सम्भव हो उतना करने-कराने की ढील देकर क्रम को प्रकार गतिशील रखा जा सकता है।
रुग्णता, दुर्बलता से ग्रसित व्यक्ति स्नान की सुविधा न होने पर हाथ-पैर, मुँह धोकर काम चला सकते हैं। गीले तौलिए से शरीर पोंछ लेना भी आधा स्नान माना जाता है। वस्त्र धुले न हों तो ऊनी कपड़े पहन कर समझा जा सकता है कि उनके धुले न होने पर भी काम चल सकता है। यों मैल पसीना तो ऊन को भी स्पर्श करता है और उन्हें भी धोने की या धूप में सुखाने की आवश्यकता पड़ती है, पर चूँकि उनके बाल गन्दगी को अपने अन्दर नहीं सोखते वह बाहर ही चिपक रह जाती है। इस दृष्टि से उसमें अशुद्ध का सम्पर्क कम होने के कारण बिना धुले होने पर भी ऊनी वस्त्र पवित्र माने जाते हैं। यों स्वच्छता की दृष्टि से वे भी ऐसे नहीं होते कि बिना धुले होने पर भी सदा प्रयुक्त किये जाते और स्वच्छ माने जाते रहें। इसलिए इतना ही कहा जा सकता है कि व्यक्ति कि असुविधा को ध्यान में रखते हुए शरीर और वस्त्रों की स्वच्छता के सम्बन्ध में उतनी ही छूट देनी चाहिए जिसके बिना काम न चलता हो। अश्रद्धा, उपेक्षा, आलस्य प्रमादवश स्वच्छता को अनावश्यक मानना और ऐसी मनमानी करना उचित नहीं।
रेशमी वस्त्रों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही मान्यता है कि उन्हें धोने की आवश्यकता नहीं। वे बिना धोये ही सुद्ध होते हैं। यह मान्यता गलत है। सूत जितनी सोखने की शक्ति न होने से अपेक्षाकृत उसमें अशुद्धि का प्रवेश कम होता है, यह माना जा सकता है, पर उसे सदा सर्वदा के लिए पवित्र मान लिया जाय और धोया ही न जाए यह गलत है धोने के समय तो सूती कपड़े की उपेक्षा कुछ अधिक किया जा सकता है, इतना भर ही माना जाना जाना चाहिए। धोया उसे भी जाय।
अब कठिनाईवश इस व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि शास्त्रकारों ने कठिनाई की स्थिति में लचीली नीति रखी है। ऐसे कड़े प्रतिबन्ध नहीं लगाएं जिनके कारण स्नान एवं धुले वस्त्र की व्यवस्था न बन पड़ने पर जप जैसा पुनीत कार्य भी बन्द कर दिया जाय। उसमें तो दुहरी हानि हुई। नियम इसलिए बने थे कि उपासना काल में अधिकतम पवित्रता रखने का प्रयत्न किया जाए। यदि नियम इतना कड़ा हो जाय कि स्नानदि न बन पड़ने पर जप, साधना का उपार्जन ही बन्द हो जाय तब बात उल्टी हो गई। नियमों की कड़ाई ने ही साधना, उपासना कृत्य से वंचित करके, कठिनाई का हल निकालने के स्थान पर रही बची संभावना भी समाप्त कर दी। जो आधा-अधूरा लाभ मिल सकता था उसकी सम्भावना भी समाप्त हो गई।
शास्त्र-विधान यह है कि शरीर, वस्त्र, पात्र, उपासना, पूजा, सामग्री, देव प्रतिमा, आसन, स्नान आदि सभी को अधिकतम स्वच्छ बनाकर उपासना कृत्य करने पर जोर दिया जाए। इसमें आलस्य-प्रमाद को हटाने और स्वच्छता को उपासना का अंग मानने की बात कही गई है। फिर भी कारणवश ऐसी कठिनाइयाँ हो सकती है, जिसमें साधक की मन-स्थिति और परिस्थिति पर ध्यान देते हुए विधान-प्रक्रिया को उस सीमा तक ढीला किया जाय, जितना किए बिना गाड़ी रुक जाने का खतरा हो। स्वच्छता की नीति पूरी तरह तो समाप्त नहीं करनी चाहिए, पर जहां तक अधिकाधिक सम्भव हो उतना करने-कराने की ढील देकर क्रम को प्रकार गतिशील रखा जा सकता है।
रुग्णता, दुर्बलता से ग्रसित व्यक्ति स्नान की सुविधा न होने पर हाथ-पैर, मुँह धोकर काम चला सकते हैं। गीले तौलिए से शरीर पोंछ लेना भी आधा स्नान माना जाता है। वस्त्र धुले न हों तो ऊनी कपड़े पहन कर समझा जा सकता है कि उनके धुले न होने पर भी काम चल सकता है। यों मैल पसीना तो ऊन को भी स्पर्श करता है और उन्हें भी धोने की या धूप में सुखाने की आवश्यकता पड़ती है, पर चूँकि उनके बाल गन्दगी को अपने अन्दर नहीं सोखते वह बाहर ही चिपक रह जाती है। इस दृष्टि से उसमें अशुद्ध का सम्पर्क कम होने के कारण बिना धुले होने पर भी ऊनी वस्त्र पवित्र माने जाते हैं। यों स्वच्छता की दृष्टि से वे भी ऐसे नहीं होते कि बिना धुले होने पर भी सदा प्रयुक्त किये जाते और स्वच्छ माने जाते रहें। इसलिए इतना ही कहा जा सकता है कि व्यक्ति कि असुविधा को ध्यान में रखते हुए शरीर और वस्त्रों की स्वच्छता के सम्बन्ध में उतनी ही छूट देनी चाहिए जिसके बिना काम न चलता हो। अश्रद्धा, उपेक्षा, आलस्य प्रमादवश स्वच्छता को अनावश्यक मानना और ऐसी मनमानी करना उचित नहीं।
रेशमी वस्त्रों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही मान्यता है कि उन्हें धोने की आवश्यकता नहीं। वे बिना धोये ही सुद्ध होते हैं। यह मान्यता गलत है। सूत जितनी सोखने की शक्ति न होने से अपेक्षाकृत उसमें अशुद्धि का प्रवेश कम होता है, यह माना जा सकता है, पर उसे सदा सर्वदा के लिए पवित्र मान लिया जाय और धोया ही न जाए यह गलत है धोने के समय तो सूती कपड़े की उपेक्षा कुछ अधिक किया जा सकता है, इतना भर ही माना जाना जाना चाहिए। धोया उसे भी जाय।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book