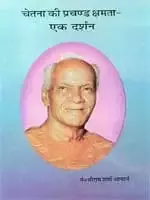|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> चेतना की प्रचण्ड क्षमता-एक दर्शन चेतना की प्रचण्ड क्षमता-एक दर्शनश्रीराम शर्मा आचार्य
|
358 पाठक हैं |
||||||
चेतना की प्रचण्ड क्षमता
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
शरीर रचना से लेकर मनःसंस्थान और अंतःकरण की भाव संवेदनाओं तक सर्वत्र
असाधारण ही दृष्टिगोचर होता है, यह सोद्देश्य होना चाहिए अन्यथा एक ही घटक
पर कलाकार का इतना श्रम और कौशल नियोजित होने की क्या आवश्यकता थी।
पौधे और मनुष्य के बीच पाये जाने वाले अंतर दृष्टिपात करने से दोनों के बीच हर क्षेत्र में मौलिक अंतर पर दृष्टिगत होता है। विशिष्टता मानवी काया के रोम-रोम में संव्याप्त है। आत्मिक गरिमा पर विचार न भी किया जाए, तो भी मात्र कार्य संरचना और उसकी क्षमता पर विचार करें तो भी इस क्षेत्र में कम अद्भुत नहीं है।
पौधे और मनुष्य के बीच पाये जाने वाले अंतर दृष्टिपात करने से दोनों के बीच हर क्षेत्र में मौलिक अंतर पर दृष्टिगत होता है। विशिष्टता मानवी काया के रोम-रोम में संव्याप्त है। आत्मिक गरिमा पर विचार न भी किया जाए, तो भी मात्र कार्य संरचना और उसकी क्षमता पर विचार करें तो भी इस क्षेत्र में कम अद्भुत नहीं है।
देव-मन्दिर के देवता और परमात्मा
‘‘स्वार्गादि उच्च लोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल आदि की
उत्पत्ति
हो चुकी तब परमात्मा ने लोकपालों की रचना का विचार किया। इस रचना का विचार
आते ही उन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश अणु पैदा किये। यह अणु अंडाकार थे और
उसमें पुरुष के लक्षण थे, फिर उस अण्ड में परमात्मा ने छेद किया जो मुख
बना, मुख से वाणी, वाणी से अग्नि उत्पन्न हुई। इसके बाद दो छेद किये, जो
नासिका कहलाये। उससे प्राण की उत्पत्ति हुई, प्राणों से वायु और नेत्रों
के छिद्र बने। इनमें सुनने की शक्ति उत्पन्न हुई, श्रोत्रेंद्रिय के
द्वारा दिशायें प्रकटीं, फिर त्वचा उत्पन्न हुई। त्वचा में रोम-रोम से
औषधियाँ, फिर हृदय, हृदय से मन और मन से चन्द्रमा प्रकट हुआ। फिर नाभि
बनी, नाभि से अपान देवता, उससे मृत्यु देवता प्रकट हुए। फिर उपस्थ, उपस्थ
से रेत, रेत से जल की उत्पत्ति हुई।’’
‘‘इस प्रकार उत्पन्न हुए देवतागण अभी तक अपने सूक्ष्म रूप में थे। परमात्मा ने उनमें भूख और प्यास की अनुभूति भी उत्पन्न कर दी थी, किन्तु वे संसार-समुद्र में निराश्रय पड़े थे, उन्हें रहने के लिए योग्य स्थान का अभाव खटक रहा था। उसके लिए उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की, तब परमात्मा ने उन्हें गाय का शरीर दिखाया। उस शरीर को देवताओं ने पसन्द नहीं किया। तब फिर उन्हें घोड़े का शरीर दिखाया, वह भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। बहुत से शरीर विधाता ने देवताओं को दिखाये, वे उन्हें पसन्द न आये, तब उसने मनुष्य शरीर दिखाया। यह देवताओं को पसन्द आ गया। अग्नि उसमें वाणी बनकर घुस गया, वायु प्राण बनकर नासिका में, सूर्य चक्षु बनकर नेत्र गोलकों में प्रविष्टं हुआ, दिशायें क्षेत्र बनकर कानों में घुसी, औषधि रोम बनकर त्वचा में पहुँची, चन्द्रमा मन बनकर हृदय में स्थित हुआ, मृत्यु अपान बनकर नाभि में, जल (रेत) बनकर उपस्थ में स्थित हो गया।’’
‘‘शरीर की यहाँ तक की रचना में पूरी तरह प्रकृति का ही आधिपत्य था, देवताओं की प्रतिष्ठा होने के कारण शरीर देवमंदिर तो बन गया, पर उसमें निवास करने वाली मूर्तियाँ- देवशक्तियाँ एक नहीं- अनेक नहीं- अनेक थीं, सबकी अपनी-अपनी आकांक्षाएँ, अपनी-अपनी वासनाएँ थीं। भगवान् ने विचार किया। यदि इन सभी देवताओं ने केवल अपनी वासनायें तृप्त करनी चाहीं, तब तो यह शरीर एक भी दिन न चल सकेगा। देवतागण उसे नष्ट कर डालेंगे। फिर इनके लिए मेरा भी तो कुछ अस्तित्व होना चाहिए, अन्यथा वे मुझे कैसे जानेंगे ? इस विचार के आते ही उसने मनुष्य शरीर की मूर्धा (शरीर का वह भाग-जहाँ से दाहिने-बायें भाग बराबर-बराबर विभक्त होते हैं, चोटी वाले स्थान से लेकर यह स्थान नीचे चूतड़ों तक के सीवन वाले भाग तक चला जाता है।) से प्रवेश किया। अब मनुष्य ने देखा कि मुझ में पांच भौतिक प्रकृति के अतिरिक्त यह बुद्धि रूप में कौन आ गया- तब उसने परमात्मा को पहचाना और उनके दर्शन पाकर स्वर्गीय सुख में विभोर हो गया।’’
ऐतरेय उपनिषद् की इस आख्यायिका में जहाँ सृष्टि के विकास का सूक्ष्म विज्ञान भरा पड़ा है, वहाँ ईश्वर दर्शन का महत्त्वपूर्ण तत्त्वदर्शन भी। सामान्य दृष्टि से देखने पर इंद्रियाँ ही मनुष्य शरीर में सक्रिय दिखाई देती हैं, इसलिए अज्ञानग्रस्त लोग दिन-रात उन्हीं की तृप्ति में जुटे रहकर मनुष्य देह रूपी मंदिर को भग्न और गंदा किया करते हैं। देवताओं को स्थूल पूजा मिलनी चाहिए, पर यदि देवताओं की संतुष्टि ही एक मात्र शरीर का उद्देश्य रह जायेगा तो उस परमात्मा की प्राप्ति के आनंद का क्या होगा ? जो इन सभी शक्तियों को भी उत्पन्न करने वाला आनंद और सृष्टि का मूल है। सारी परिपूर्णतायें तो एक मात्र ब्रह्म में ही हैं, उसे प्राप्त किये बिना आत्मिक सुख कहाँ ?
परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए ? यह संसार के सामने जटिल और गंभीर प्रश्न है ? ऐतरेय उपनिषद् इस प्रश्न की हलकी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण शोध है। इससे तथ्यों को बड़े सरल ढंग से समझाया गया है, यह बताया गया है कि इंद्रियों की वासनायें मनुष्य की आवश्यकताएँ नहीं वरन् देवशक्तियों की आकांक्षायें होती हैं। मनुष्य तो बुद्धि, ज्ञान और चेतना को कहते हैं। बुद्धि परमात्मा की प्रतिनिधि है अर्थात् मनुष्य देवशक्तियों से ऊपर की सत्ता है। उसे इंद्रियों का स्वामी बनकर देवशक्तियों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी बौद्धिक एवं आत्मिक क्षमताओं का विकास करके विराट् ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही परम पुरुषार्थ है और यही है योग। जो अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया है, उसे अपने लघु रूप को विराट् ब्रह्म में परिवर्तित करते देर न लगेगी।
अभी तक यह ज्ञान केवल शास्त्रों तक सीमित था। शास्त्रीय व्याख्याओं से विश्वास उठ जाने के कारण इस तरह के विवेचनों के प्रति अश्रद्धालु होना और इस तरह जीवन-विकास के मूल-ज्ञान से वंचित रह जाना स्वाभाविक ही था। इसे अपना दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि हमारे देशवासी स्वयं इस महत्तम विज्ञान को भूल गये, जिसका प्रतिपादन आज भौतिक-विज्ञान भी करता है।
शरीर विज्ञान मानता है कि मनुष्य का मस्तिष्क इंद्रियों की सामर्थ्य से बड़ा और उनका स्वामी है, अतएव इंद्रियों को नहीं, महत्त्व बौद्धिक शक्तियों को देना चाहिए। इस दृष्टि से मस्तिष्क की बारह नसों और सात शून्य स्थानों (सात-लोक) की शोध एक विशिष्ट महत्त्व रखती है। यह नसे मस्तिष्क के निचले वाले धरातल से निकलती हैं और शरीर के सभी तन्मात्रा अवयवों तक चली जाती हैं।
(1) आलफैक्ट्री नस का संबंध नासिका नली से है, जिससे मस्तिष्क सूँघने की अनुभूति करता है।
(2) ऑप्टिक नस नेत्र गोलको तक चली जाती है और वही मस्तिष्क को सामने वाली वस्तुओं का ज्ञान कराती है।
(3) आकुलोमोटर का संबंध भी आँखों से है, इससे पुतलियों को गति मिलती है।
(4) ट्रॉक्लियर नेत्र की मांस-पेशियों को जोड़ने वाली नस है।
(5) ट्राइजैमिनल मुख के निचले जबड़े एवं जीभ की मांस-पेशियों से संबंध जोड़ती है और स्वाद आदि की अनुभूति में सहायक होती है।
(6) ऐब्ड्यूसेन्ट आँख को बाहर की ओर खींचे रहती है।
(7) फेसियल मुख की मांस-पेशियों को।
(8) ऑडिटरी-कानों में।
(9) ग्लासोफेरिब्जयल स्वरध्वनि यंत्र (लेरिंग्स), जीभ व गले को मस्तिष्क के उस चमत्कारी अवचेतन अंश से जोड़ते हैं।
(10) स्पाइनल ऐक्सेसरी गले की बाहरी ऐच्छिक मांसपेशियों को क्रियाशीलता प्रदान करती है।
(11) वेगस अंदर का गला, स्वरध्वनि यंत्र, फेफड़े, हृदय व पाचन संस्थान को सप्लाई करती है और
(12) हाइपोग्लोसल जीभ की मांस-पेशियों को। इसके अतिरिक्त सुषुम्ना शार्ष जो कि लगभग संपूर्ण मेरुदण्ड है, मस्तिष्क का संबंध सीधे प्रजनन केन्द्रों से जोड़ती है।
आधुनिक शरीर वैज्ञानिकों का ज्ञान अधिकांश शरीर के स्थूल अवयवों तक सीमित है। चेतना की आंतरिक अनुभूतियों का ज्ञान वे नहीं कर सके, इसलिए जीवात्मा के दार्शनिक पक्ष को इनमें से कोई भी प्रमाणित करने में आज तक सफल नहीं हुआ। उदाहरणार्थ- आकुलोमोटर का संबंध मस्तिष्क से त्रिकुटी मध्य के उस भाग से है, जहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, पर शरीर रचना शास्त्री उसे केवल दोनों पुतलियों से संबंधित मानते हैं। स्पाइनस एक्सेसरी नाभि स्थित सूर्य चक्र (सोलर प्लैक्सस) से संबंधित है और योग विद्या में उसका अपना विशिष्ट महत्त्व है, पर उसे भी शरीर-रचना शास्त्री नहीं जानते।
यहाँ तक कि नाभि जैसे महत्त्वपूर्ण संस्थान के बारे में, जिससे कि गर्भवस्था में सारे शरीर को पोषण मिलता है, वैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते हैं, तो यह कम महत्त्वपूर्ण नहीं कि उन्होंने इन जानकारियों के आधार पर इतना तो सिद्ध कर ही दिया कि मस्तिष्क ही संपूर्ण इंद्रियों का अधिष्ठान है। यदि मस्तिष्क नहीं रहता तो इन सभी इंद्रियों को चेतना अपना कारोबार समेटकर उसे नष्ट कर देने में ही जुट जाती और अपनी समस्त सूक्ष्म तन्मात्राओं को मस्तिष्क में ही केन्द्रित कर देती, यही मस्तिष्कीय चेतना इंद्रिय सूक्ष्म तन्मात्रायें को लेकर मृत्यु काल में शरीर से विदा होकर फिर दूसरी योनियों की तालाश में चली जाती है और क्रम जब तक चलता रहता है, जब तक मस्तिष्कीय द्रव्य प्रकृति के अज्ञान आवरण और इंद्रियों की लिप्साओं को स्वच्छ नहीं कर लेता। यजुर्वेद में इसी तथ्य को दोहराते हुए ऋषि ने लिखा है-
‘‘इस प्रकार उत्पन्न हुए देवतागण अभी तक अपने सूक्ष्म रूप में थे। परमात्मा ने उनमें भूख और प्यास की अनुभूति भी उत्पन्न कर दी थी, किन्तु वे संसार-समुद्र में निराश्रय पड़े थे, उन्हें रहने के लिए योग्य स्थान का अभाव खटक रहा था। उसके लिए उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की, तब परमात्मा ने उन्हें गाय का शरीर दिखाया। उस शरीर को देवताओं ने पसन्द नहीं किया। तब फिर उन्हें घोड़े का शरीर दिखाया, वह भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। बहुत से शरीर विधाता ने देवताओं को दिखाये, वे उन्हें पसन्द न आये, तब उसने मनुष्य शरीर दिखाया। यह देवताओं को पसन्द आ गया। अग्नि उसमें वाणी बनकर घुस गया, वायु प्राण बनकर नासिका में, सूर्य चक्षु बनकर नेत्र गोलकों में प्रविष्टं हुआ, दिशायें क्षेत्र बनकर कानों में घुसी, औषधि रोम बनकर त्वचा में पहुँची, चन्द्रमा मन बनकर हृदय में स्थित हुआ, मृत्यु अपान बनकर नाभि में, जल (रेत) बनकर उपस्थ में स्थित हो गया।’’
‘‘शरीर की यहाँ तक की रचना में पूरी तरह प्रकृति का ही आधिपत्य था, देवताओं की प्रतिष्ठा होने के कारण शरीर देवमंदिर तो बन गया, पर उसमें निवास करने वाली मूर्तियाँ- देवशक्तियाँ एक नहीं- अनेक नहीं- अनेक थीं, सबकी अपनी-अपनी आकांक्षाएँ, अपनी-अपनी वासनाएँ थीं। भगवान् ने विचार किया। यदि इन सभी देवताओं ने केवल अपनी वासनायें तृप्त करनी चाहीं, तब तो यह शरीर एक भी दिन न चल सकेगा। देवतागण उसे नष्ट कर डालेंगे। फिर इनके लिए मेरा भी तो कुछ अस्तित्व होना चाहिए, अन्यथा वे मुझे कैसे जानेंगे ? इस विचार के आते ही उसने मनुष्य शरीर की मूर्धा (शरीर का वह भाग-जहाँ से दाहिने-बायें भाग बराबर-बराबर विभक्त होते हैं, चोटी वाले स्थान से लेकर यह स्थान नीचे चूतड़ों तक के सीवन वाले भाग तक चला जाता है।) से प्रवेश किया। अब मनुष्य ने देखा कि मुझ में पांच भौतिक प्रकृति के अतिरिक्त यह बुद्धि रूप में कौन आ गया- तब उसने परमात्मा को पहचाना और उनके दर्शन पाकर स्वर्गीय सुख में विभोर हो गया।’’
ऐतरेय उपनिषद् की इस आख्यायिका में जहाँ सृष्टि के विकास का सूक्ष्म विज्ञान भरा पड़ा है, वहाँ ईश्वर दर्शन का महत्त्वपूर्ण तत्त्वदर्शन भी। सामान्य दृष्टि से देखने पर इंद्रियाँ ही मनुष्य शरीर में सक्रिय दिखाई देती हैं, इसलिए अज्ञानग्रस्त लोग दिन-रात उन्हीं की तृप्ति में जुटे रहकर मनुष्य देह रूपी मंदिर को भग्न और गंदा किया करते हैं। देवताओं को स्थूल पूजा मिलनी चाहिए, पर यदि देवताओं की संतुष्टि ही एक मात्र शरीर का उद्देश्य रह जायेगा तो उस परमात्मा की प्राप्ति के आनंद का क्या होगा ? जो इन सभी शक्तियों को भी उत्पन्न करने वाला आनंद और सृष्टि का मूल है। सारी परिपूर्णतायें तो एक मात्र ब्रह्म में ही हैं, उसे प्राप्त किये बिना आत्मिक सुख कहाँ ?
परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए ? यह संसार के सामने जटिल और गंभीर प्रश्न है ? ऐतरेय उपनिषद् इस प्रश्न की हलकी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण शोध है। इससे तथ्यों को बड़े सरल ढंग से समझाया गया है, यह बताया गया है कि इंद्रियों की वासनायें मनुष्य की आवश्यकताएँ नहीं वरन् देवशक्तियों की आकांक्षायें होती हैं। मनुष्य तो बुद्धि, ज्ञान और चेतना को कहते हैं। बुद्धि परमात्मा की प्रतिनिधि है अर्थात् मनुष्य देवशक्तियों से ऊपर की सत्ता है। उसे इंद्रियों का स्वामी बनकर देवशक्तियों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी बौद्धिक एवं आत्मिक क्षमताओं का विकास करके विराट् ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही परम पुरुषार्थ है और यही है योग। जो अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया है, उसे अपने लघु रूप को विराट् ब्रह्म में परिवर्तित करते देर न लगेगी।
अभी तक यह ज्ञान केवल शास्त्रों तक सीमित था। शास्त्रीय व्याख्याओं से विश्वास उठ जाने के कारण इस तरह के विवेचनों के प्रति अश्रद्धालु होना और इस तरह जीवन-विकास के मूल-ज्ञान से वंचित रह जाना स्वाभाविक ही था। इसे अपना दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि हमारे देशवासी स्वयं इस महत्तम विज्ञान को भूल गये, जिसका प्रतिपादन आज भौतिक-विज्ञान भी करता है।
शरीर विज्ञान मानता है कि मनुष्य का मस्तिष्क इंद्रियों की सामर्थ्य से बड़ा और उनका स्वामी है, अतएव इंद्रियों को नहीं, महत्त्व बौद्धिक शक्तियों को देना चाहिए। इस दृष्टि से मस्तिष्क की बारह नसों और सात शून्य स्थानों (सात-लोक) की शोध एक विशिष्ट महत्त्व रखती है। यह नसे मस्तिष्क के निचले वाले धरातल से निकलती हैं और शरीर के सभी तन्मात्रा अवयवों तक चली जाती हैं।
(1) आलफैक्ट्री नस का संबंध नासिका नली से है, जिससे मस्तिष्क सूँघने की अनुभूति करता है।
(2) ऑप्टिक नस नेत्र गोलको तक चली जाती है और वही मस्तिष्क को सामने वाली वस्तुओं का ज्ञान कराती है।
(3) आकुलोमोटर का संबंध भी आँखों से है, इससे पुतलियों को गति मिलती है।
(4) ट्रॉक्लियर नेत्र की मांस-पेशियों को जोड़ने वाली नस है।
(5) ट्राइजैमिनल मुख के निचले जबड़े एवं जीभ की मांस-पेशियों से संबंध जोड़ती है और स्वाद आदि की अनुभूति में सहायक होती है।
(6) ऐब्ड्यूसेन्ट आँख को बाहर की ओर खींचे रहती है।
(7) फेसियल मुख की मांस-पेशियों को।
(8) ऑडिटरी-कानों में।
(9) ग्लासोफेरिब्जयल स्वरध्वनि यंत्र (लेरिंग्स), जीभ व गले को मस्तिष्क के उस चमत्कारी अवचेतन अंश से जोड़ते हैं।
(10) स्पाइनल ऐक्सेसरी गले की बाहरी ऐच्छिक मांसपेशियों को क्रियाशीलता प्रदान करती है।
(11) वेगस अंदर का गला, स्वरध्वनि यंत्र, फेफड़े, हृदय व पाचन संस्थान को सप्लाई करती है और
(12) हाइपोग्लोसल जीभ की मांस-पेशियों को। इसके अतिरिक्त सुषुम्ना शार्ष जो कि लगभग संपूर्ण मेरुदण्ड है, मस्तिष्क का संबंध सीधे प्रजनन केन्द्रों से जोड़ती है।
आधुनिक शरीर वैज्ञानिकों का ज्ञान अधिकांश शरीर के स्थूल अवयवों तक सीमित है। चेतना की आंतरिक अनुभूतियों का ज्ञान वे नहीं कर सके, इसलिए जीवात्मा के दार्शनिक पक्ष को इनमें से कोई भी प्रमाणित करने में आज तक सफल नहीं हुआ। उदाहरणार्थ- आकुलोमोटर का संबंध मस्तिष्क से त्रिकुटी मध्य के उस भाग से है, जहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, पर शरीर रचना शास्त्री उसे केवल दोनों पुतलियों से संबंधित मानते हैं। स्पाइनस एक्सेसरी नाभि स्थित सूर्य चक्र (सोलर प्लैक्सस) से संबंधित है और योग विद्या में उसका अपना विशिष्ट महत्त्व है, पर उसे भी शरीर-रचना शास्त्री नहीं जानते।
यहाँ तक कि नाभि जैसे महत्त्वपूर्ण संस्थान के बारे में, जिससे कि गर्भवस्था में सारे शरीर को पोषण मिलता है, वैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते हैं, तो यह कम महत्त्वपूर्ण नहीं कि उन्होंने इन जानकारियों के आधार पर इतना तो सिद्ध कर ही दिया कि मस्तिष्क ही संपूर्ण इंद्रियों का अधिष्ठान है। यदि मस्तिष्क नहीं रहता तो इन सभी इंद्रियों को चेतना अपना कारोबार समेटकर उसे नष्ट कर देने में ही जुट जाती और अपनी समस्त सूक्ष्म तन्मात्राओं को मस्तिष्क में ही केन्द्रित कर देती, यही मस्तिष्कीय चेतना इंद्रिय सूक्ष्म तन्मात्रायें को लेकर मृत्यु काल में शरीर से विदा होकर फिर दूसरी योनियों की तालाश में चली जाती है और क्रम जब तक चलता रहता है, जब तक मस्तिष्कीय द्रव्य प्रकृति के अज्ञान आवरण और इंद्रियों की लिप्साओं को स्वच्छ नहीं कर लेता। यजुर्वेद में इसी तथ्य को दोहराते हुए ऋषि ने लिखा है-
यस्य प्रयाण मन्वन्यऽ इद्ययुर्देवा देवस्य महिमान मोजसा।
य: पार्थिवानि विममे स एतशो रजाँसि देव: सविता महित्वना।
य: पार्थिवानि विममे स एतशो रजाँसि देव: सविता महित्वना।
यजुर्वेद 11/6
अर्थात्- दूसरे सभी देवता (इंद्रियाँ) जिस देवता (जीवात्मा) के अधीन गति
करती हैं। जब जीवात्मा शरीर त्याग देता है तो उसी के अधीन गति करती हैं।
जब जीवात्मा शरीर त्याग देता है तो उसी के अधीन चली जाती हैं। जिस देवता
(जीवात्मा) की यह ओजस-शक्तियाँ उन्हीं के अनुरूप बन जाती हैं। यह श्रेष्ठ
योनियों को प्राप्त होकर मुक्ति का स्वामी बनता है अन्यथा निम्नगामी
योनियों में चला जाता है। इस प्रकार जीवात्मा के बड़प्पन के लिए प्राप्त
हुई इंद्रियाँ ही उसे दुर्गति में ले जाने वाली अथवा मुक्ति में सहायक
होती हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book