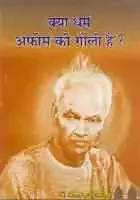|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> क्या धर्म अफीम की गोली है ? क्या धर्म अफीम की गोली है ?श्रीराम शर्मा आचार्य
|
210 पाठक हैं |
||||||
क्या धर्म अफीम की गोली नहीं ?....
धर्म एक परिष्कृत दृष्टिकोण
प्राचीन भारत के मनीषियों ने धर्म का अर्थ व्यापक माना है। ऋषि-मुनियों ने वर्ग-संप्रदाय आदि केभेदभाव के बिना प्राणिमात्र के कल्याण के निमित्त ज्ञान-विज्ञान का अन्वेषण किया। जप-तप की अनुभूतियों से विश्वमानव को लाभान्वित करने केसूत्र और मंत्रों की रचना की। वेद-वेदांग इसका ज्वलंत प्रमाण है।
वेद को धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। उसमें समग्र जीवन जीने की कला का वर्णन मिलता है।व्यक्तिगत ही नहीं, सामाजिक समस्याओं का समाधान है। आध्यात्मिक ही नहीं, अपितु आर्थिक, राजनीतिक विषय भी हैं। शासन प्रणाली के प्रसंग में‘साम्राज्य भोज्यं स्वराज्यं वराज्यं पारमेष्ठयं राज्यम्' आदि ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है।
हमारा कोई धर्मग्रंथ एकांगी नहीं। धर्मशास्त्रों में भी सर्वांगीण विधि बताई गई है।धर्म की परिभाषा है'यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।'' ऐहलौकिक अभ्युदय भला भौतिक,आर्थिक,सामाजिक, राजनीतिक ज्ञान शून्यता से कैसे संभवहै ? धर्म परमार्थ के साथ पुरुषार्थ सिखाता है। आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए कहकर जीवन को पूर्णता प्रदान करता है।
आज लोग हिंदू, मुसलिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि को धर्म मानने लगे हैं। अतः इनसेभेदभाव रहित होना' धर्म-निरपेक्षता कहलाता है। यह भ्रामक और गलत दृष्टिकोण है। मुसलिम, यहूदी, मसीही आदि संप्रदाय हैं, धर्म नहीं। धर्म तो एकांगीपथ-संप्रदायों से भी ऊपर है, संप्रदाय जलबिंदु के समान हैं, धर्म समुद्र है। संप्रदायातीत जीवन ही मानवता का स्वरूप है।
परंतु वर्तमान विश्व में जितनी विचारधाराएँ जोरों पर फैल रही हैं, उनमें कृत्रिमता औरअधूरा दर्शन है। कुछ एकांगी विचार प्रतिक्रियात्मक और कुछ नकली हैं। पूँजीवाद एकांगी विचार है। पूँजीवाद की प्रतिक्रियास्वरूप साम्यवाद है।भारत में प्रचलित अन्य कई धारणाएँ तो अँगरेजों की सीधी नकल हैं। इस तरह के विचार उस काल में चलते हैं, फिर थोड़े समय के बाद खतम हो जाते हैं।
इस युग की यही विडंबना है कि उद्योग और विज्ञान के विकास से हमारा दृष्टिकोण भौतिकवादीऔर स्वार्थपरायण बन गया है। अनास्था और अविश्वास के कारण धार्मिक दर्शन के प्रति द्वंद्व उत्पन्न हुआ। विद्या-विहीन शिक्षित और साधनसंपन्न लोग यहसमझते हैं। कि नए समाज के निर्माण की शक्ति धर्म में रही नहीं। धर्मतत्त्व के प्रति अश्रद्धा और उपेक्षा इसी अज्ञान की उपज है।
यद्यपि विभिन्न मत-पंथ, संप्रदाय और वादों का प्रारंभ व्यक्तिगत तथा समष्टिगत भूलों कोसुधारने की दृष्टि से होता है। व्यक्ति का कल्याण एवं सुंदर समाज का निर्माण ही सभी मत वादों का मुख्य उद्देश्य है, किंतु उनकी ममता व्यक्तिको पागल बना देती है। यही भ्रांति और मोह कहलाता है। हम भूल जाते हैं कि ओषधि का सेवन आरोग्य के लिए है, ममता, किंवा, आसक्ति हेतु नहीं। सभी धर्मविचारों से स्वयं एवं समाज को सुंदर तथा आनंददायक बनाने की अपेक्षा की जाती है।
जिस दृष्टिकोण की गला फाड़-फाड़कर प्रशंसा की जाती है। यदि वह विश्व-कल्याण हेतुजीवात्मा को सन्मार्ग पर चलाने में उपयोगी न बन सका तो उसका परिर्वतन स्वाभाविक है। प्रेम, सत्य और यथार्थ ही धर्म है। एकता और समता का मूल यहीधार्मिक दृष्टिकोण है। धर्म का नया दृष्टिकोण इसी सार्वभौम धर्म का प्रतिपादन करता है।
अनुपयोगी मतवाद और सांप्रदायिक भेदभाव तथा पाखंड को भुलाकर धर्म के इस नए दृष्टिकोण कोजीवन व्यवहार में क्रियान्वित करना ही पड़ेगा। अन्यथा अधर्म, अनास्था, अभाव, दुर्भाव के कारण विविध समस्याजनित संकट समूची मानव सभ्यता के विनाशका चित्र प्रस्तुत कर देगा।
हम जानते हैं कि मानवमात्र के अत:करण में धर्म का देवी भाव भी विद्यमान है। प्रयोजन है,परम सत्य की अनुभूति का अमृत पिलाकर आत्मपरिचय कराने का-अखण्ड ज्योति जलाकर सद्ज्ञान के अनुदान से सद्भाव जागरण का।
जीवात्मा का ध्येय है-अनंत आनंद की प्राप्ति। ‘मृत्योर्मा अमृतम् गमय' मैं इसी अमरताकी माँग है। नदियाँ अपने आप में संतुष्ट न होने से समुद्र की ओर दौड़ी चली जाती हैं। हवा को एक स्थान पर चैन नहीं। यह प्रतिक्रिया संसार के प्रत्येकपरमाणु में चल रही है। किसी को भी अपने आप में संतोष नहीं मिलता। जड़ व चेतन सभी पूर्णता के लिऐ गतिवान हैं। अपने स्वत्व को किसी महान सत्ता मेंघुला देने के लिए सबके सब सतत क्रियाशील दिखाई देते हैं।
ऐसी ही प्रक्रिया जीवात्मा की है। व्यष्टि में उसे अनंत आनंद की प्राप्ति नहीं।समष्टि की परमात्मा के पावन स्पर्श हेतु सेवा-भक्ति अनिवार्य है। आत्मचिंतन की प्रवृति से जीवन-मरण के रहस्य का अनावरण होता है। उसे यहआभास मिलता है कि मानव को यहाँ वे सारी परिस्थितियाँ प्राप्त हैं, जिनके सहारे सक्रिय होने पर वह अपनी विकास-यात्रा आसानी से पूरी कर सकता है।
परमात्मा से प्रेम एवं आत्मीयता स्थापित करने का अच्छा तरीका यह है कि हम उसका अभ्यासपरिजनों से प्रारंभ करें। संसार में सबके साथ सत्य का व्यवहार करें, न्याय रखें और सहिष्णुता बरतें। स्वार्थ की अहंवृति का परित्याग कर परमार्थ केविशाल क्षेत्र में पदार्पण करें। इससे मनुष्य विराट की ओर अग्रसर होता है। यही नया दृष्टिकोण युग की अनिवार्य आवश्यकता है।
ऐसे धार्मिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हजारों-लाखों योनियों के बाद सौभाग्य से उपलब्धमानव जीवन को तुच्छ स्वार्थमय गोरखधंधों में ही दुरुपयोग करने की मूर्खता नहीं करेगा। यह प्रत्यक्ष है। कि पशु-पक्षी की तुलना में ज्ञान या धर्मभावना के कारण ही वह श्रेष्ठ है।
धर्म का मूलोद्देश्य है जीवन को आध्यात्मिक दिशा में मोड़ते हुए उस परम लक्ष्य कोप्राप्त करना। आस्तिकता का अवलंबन लेकर क्रमशः उस दिशा में बढ़ा जा सकता है। धार्मिकता का तत्त्वज्ञान हमें कर्तव्यपरायण बने रहने और जीवन केसंग्राम के हर मोरचे पर लड़ाई लड़ने का शौर्य एवं साहस प्रदान करता है। धर्म में सज्जनता, शालीनता, कर्तव्यपरायणता एवं प्रखरता के वे सारे तत्त्वमौजूद हैं जिनका आश्रय लेकर कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में सुख-शांति का जीवन यापन करते हुए अपने जीवन-लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होसकता है। धार्मिक दर्शन का मूलोद्देश्य भी यही है।
|
|||||