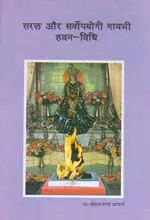|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> सरल और सर्वोपयोगी गायत्री हवन-विधि सरल और सर्वोपयोगी गायत्री हवन-विधिश्रीराम शर्मा आचार्य
|
192 पाठक हैं |
||||||
गायत्री हवन-विधि पद्धति....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्राक्कथन
गायत्री भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ भारतीय धर्म का पिता है। इन
दोनों का समन्वय ही भारतीय तत्व ज्ञान का संगम-समन्वय कहा जा सकता है।
विवेक बुद्धि की प्रतिनिधि गायत्री सद्भावनाओं और उत्कृष्ट चिन्तन को
प्रेरणा देती है। यज्ञ आत्मसंयम और उदार व्यवहार का प्रेरक है, उसमें
सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्द्धन का, आदर्श कर्तृव्य का दिशा-निर्देश है।
संक्षेप में अन्तरंग और बहिरंग जीवन को यज्ञीय परम्पराओं के अनुरूप ढालने
की रीति-नीति को हृदयंगम करने की धर्मचेष्ठा को गायत्री यज्ञ कह सकते हैं।
इस कर्मकाण्ड के माध्यम से जनमानस को मानवोचित स्तर तक ऊँचा उठा ले जाने
में बड़ी सहायता मिलती रही है। भविष्य में और भी अधिक सहायता मिल सकती है।
गायत्री यज्ञ परम्परा को अधिक विस्तृत, व्यापक और लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया है कि कर्मकाण्ड को कुछ और संक्षिप्त किया जाये, ताकि विधि-विधानों की अधिक अच्छी व्याख्या करते हुए लोकशिक्षण के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिक समय लगाया जा सके।
यह संक्षिप्तीकरण उन प्रसंगों के लिए किया गया है, जिनमें कम समय में गायत्री यज्ञ पूरा कर लेने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। महिला जागरण के साप्ताहिक सत्संगों में तथा युग निर्माण शाखाओं की साप्ताहिक गोष्ठियों में संक्षिप्त हवन क्रम चलना ही संभव है। प्रस्तुत प्रक्रिया के आधार पर प्रायः गोष्ठी का शेष समय लोकशिक्षण के अन्य प्रवचनात्मक कार्यों में प्रयुक्त हो सकता है। शुभ अवसरों पर लोग गायत्री यज्ञ को कराना चाहते हैं, पर उसमें अधिक देर लग जाने और अन्य क्रिया-कलापों के लिए समय न बचने की कठिनाई के कारण उसे छोड़ना पड़ता है। आशा है कि इस संक्षिप्तीकरण से वह कठिनाई दूर हो जायेगी। व्याख्या करने तथा आयोजन-व्यवस्था की जानकारी में भी इस नयी पुस्तिका से सहायता मिलेगी-ऐसी आशा है।
गायत्री यज्ञ परम्परा को अधिक विस्तृत, व्यापक और लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया है कि कर्मकाण्ड को कुछ और संक्षिप्त किया जाये, ताकि विधि-विधानों की अधिक अच्छी व्याख्या करते हुए लोकशिक्षण के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिक समय लगाया जा सके।
यह संक्षिप्तीकरण उन प्रसंगों के लिए किया गया है, जिनमें कम समय में गायत्री यज्ञ पूरा कर लेने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। महिला जागरण के साप्ताहिक सत्संगों में तथा युग निर्माण शाखाओं की साप्ताहिक गोष्ठियों में संक्षिप्त हवन क्रम चलना ही संभव है। प्रस्तुत प्रक्रिया के आधार पर प्रायः गोष्ठी का शेष समय लोकशिक्षण के अन्य प्रवचनात्मक कार्यों में प्रयुक्त हो सकता है। शुभ अवसरों पर लोग गायत्री यज्ञ को कराना चाहते हैं, पर उसमें अधिक देर लग जाने और अन्य क्रिया-कलापों के लिए समय न बचने की कठिनाई के कारण उसे छोड़ना पड़ता है। आशा है कि इस संक्षिप्तीकरण से वह कठिनाई दूर हो जायेगी। व्याख्या करने तथा आयोजन-व्यवस्था की जानकारी में भी इस नयी पुस्तिका से सहायता मिलेगी-ऐसी आशा है।
ब्रह्मवर्चस
भूमिका
गायत्री यज्ञ-उपयोगिता और आवश्यकता
भारतीय संस्कृति का उद्गम्, ज्ञान-गंगोत्री गायत्री ही है। भारतीय धर्म का
पिता यज्ञ को माना जाता है। गायत्री को सद्विचार और यज्ञ को सत्कर्म का
प्रतीक मानते हैं। इन दोनों का सम्मिलित स्वरूप सद्भावनाओं एवं
सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाते हुए विश्व-शांति एवं मानव कल्याण का माध्यम
बनता है और प्राणिमात्र के कल्याण की सम्भावनाएँ बढ़ती हैं।
यज्ञ शब्द के तीन अर्थ हैं—1—देवपूजा, 2—दान, 3-संगतिकरण। संगतिकरण का अर्थ है—संगठन। यज्ञ का एक प्रमुख उद्देश्य धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को सत्प्रयोजन के लिए संगठित करना भी है। इस युग में संघ शक्ति ही सबसे प्रमुख है। परास्त देवताओं को पुनः विजयी बनाने के लिए प्रजापति ने उनकी पृथक्-पृथक् शक्तियों का एकीकरण करके संघ-शक्ति के रूप में दुर्गा-शक्ति का प्रादुर्भाव किया था। उस माध्यम से उनके दिन फिरे और संकट दूर हुए। मानवजाति की समस्या का हल सामूहिक शक्ति एवं संघबद्धता पर निर्भर है, एकाकी-व्यक्तित्ववादी-असंगठित लोग दुर्बल और स्वार्थी माने जाते हैं। गायत्री यज्ञों का वास्तविक लाभ सार्वजनिक रूप से, जन सहयोग से सम्पन्न कराने पर ही उपलब्ध होता है।
यज्ञ का तात्पर्य है-त्याग, बलिदान, शुभ कर्म। अपने प्रिय खाद्य पदार्थों एवं मूल्यवान् सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित किया जाता है। वायु शोधन से सबको आरोग्यवर्धक साँस लेने का अवसर मिलता है। हवन हुए पदार्थ वायुभूत होकर प्राणिमात्र को प्राप्त होते हैं और उनके स्वार्थवर्धन, रोग निवारण में सहायक होते हैं। यज्ञ काल में उच्चारित वेद मंत्रों को पुनीत शब्द-ध्वनि आकाश में व्याप्त होकर लोगों के अंतःकरण को सात्विक एवं शुद्ध बनाती है। इस प्रकार थोड़े ही खर्च एवं प्रयत्न से यज्ञकर्ताओं द्वारा संसार की बड़ी सेवा बन पड़ती है।
वैयक्तिक उन्नति और सामाजिक प्रगति का सारा आधार सहकारिता, त्याग, परोपकार आदि प्रवृत्तियों पर निर्भर है। यदि माता अपने रक्त-मांस में से एक भाग नये शिशु का निर्माण करने के लिए न त्यागे, प्रसव की वेदना न सहे, अपना शरीर निचोड़कर उसे दूध न पिलाए, पालन-पोषण में कष्ट न उठाए और यह सब कुछ नितान्त निःस्वार्थ भाव से न करे, तो फिर मनुष्य का जीवन-धारण कर सकना भी संभव न हो। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म यज्ञ भावना के द्वारा या उसके कारण ही संभव होता है। गीताकार ने इसी तथ्य को इस प्रकार कहा है कि प्रजापति ने यज्ञ को मनुष्य के साथ जुड़वा भाई की तरह पैदा किया और यह व्यवस्था की, कि एक दूसरे का अभिवर्धन करते हुए दोनों फलें-फूलें।
यदि यज्ञ भावना के साथ मनुष्य ने अपने को जोड़ा न होता, तो अपनी शारीरिक असमर्थता और दुर्बलता के कारण अन्य पशुओं की प्रतियोगिता में यह कब का अपना अस्तित्व खो बैठा होता। यह जितना भी अब तक बढ़ा है, उसमें उसकी यज्ञ भावना ही एक मात्र माध्यम है। आगे भी यदि प्रगति करनी हो, तो उसका आधार यही भावना होगी।
प्रकृति का स्वभाव यज्ञ परंपरा के अनुरूप है। समुद्र बादलों को उदारतापूर्वक जल देता है, बादल एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे ढोकर ले जाने और बरसाने का श्रम करते हैं। नदी, नाले प्रवाहित होकर भूमि को सींचते और प्राणियों की प्यास बुझाते हैं। वृक्ष एवं वनस्पतियाँ अपने अस्तित्व का लाभ दूसरों की हो देते हैं। पुष्प और फल दूसरे के लिए ही जीते हैं। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वायु आदि की क्रियाशीलता उनके अपने लाभ के लिए नहीं, वरन् दूसरों के लिए ही है। शरीर का प्रत्येक अवयव अपने निज के लिए नहीं, वरन् समस्त शरीर के लाभ के लिए ही अनवरत गति से कार्यरत रहता है। इस प्रकार जिधर भी दृष्टिपात किया जाए, यही प्रकट होता है कि इस संसार में जो कुछ स्थिर व्यवस्था है, वह यज्ञ पर ही अवलम्बित है। यदि इसे हटा दिया जाए, तो सारे सुन्दरता कुरूपता में और सारी प्रगति विनाश में परिणत हो जायेगी। ऋषियों ने कहा है—यज्ञ ही इस संसार चक्र का धुरा है। धुरा टूट जाने पर गाड़ी का आगे बढ़ सकना कठिन है।
यज्ञ शब्द के तीन अर्थ हैं—1—देवपूजा, 2—दान, 3-संगतिकरण। संगतिकरण का अर्थ है—संगठन। यज्ञ का एक प्रमुख उद्देश्य धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को सत्प्रयोजन के लिए संगठित करना भी है। इस युग में संघ शक्ति ही सबसे प्रमुख है। परास्त देवताओं को पुनः विजयी बनाने के लिए प्रजापति ने उनकी पृथक्-पृथक् शक्तियों का एकीकरण करके संघ-शक्ति के रूप में दुर्गा-शक्ति का प्रादुर्भाव किया था। उस माध्यम से उनके दिन फिरे और संकट दूर हुए। मानवजाति की समस्या का हल सामूहिक शक्ति एवं संघबद्धता पर निर्भर है, एकाकी-व्यक्तित्ववादी-असंगठित लोग दुर्बल और स्वार्थी माने जाते हैं। गायत्री यज्ञों का वास्तविक लाभ सार्वजनिक रूप से, जन सहयोग से सम्पन्न कराने पर ही उपलब्ध होता है।
यज्ञ का तात्पर्य है-त्याग, बलिदान, शुभ कर्म। अपने प्रिय खाद्य पदार्थों एवं मूल्यवान् सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित किया जाता है। वायु शोधन से सबको आरोग्यवर्धक साँस लेने का अवसर मिलता है। हवन हुए पदार्थ वायुभूत होकर प्राणिमात्र को प्राप्त होते हैं और उनके स्वार्थवर्धन, रोग निवारण में सहायक होते हैं। यज्ञ काल में उच्चारित वेद मंत्रों को पुनीत शब्द-ध्वनि आकाश में व्याप्त होकर लोगों के अंतःकरण को सात्विक एवं शुद्ध बनाती है। इस प्रकार थोड़े ही खर्च एवं प्रयत्न से यज्ञकर्ताओं द्वारा संसार की बड़ी सेवा बन पड़ती है।
वैयक्तिक उन्नति और सामाजिक प्रगति का सारा आधार सहकारिता, त्याग, परोपकार आदि प्रवृत्तियों पर निर्भर है। यदि माता अपने रक्त-मांस में से एक भाग नये शिशु का निर्माण करने के लिए न त्यागे, प्रसव की वेदना न सहे, अपना शरीर निचोड़कर उसे दूध न पिलाए, पालन-पोषण में कष्ट न उठाए और यह सब कुछ नितान्त निःस्वार्थ भाव से न करे, तो फिर मनुष्य का जीवन-धारण कर सकना भी संभव न हो। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म यज्ञ भावना के द्वारा या उसके कारण ही संभव होता है। गीताकार ने इसी तथ्य को इस प्रकार कहा है कि प्रजापति ने यज्ञ को मनुष्य के साथ जुड़वा भाई की तरह पैदा किया और यह व्यवस्था की, कि एक दूसरे का अभिवर्धन करते हुए दोनों फलें-फूलें।
यदि यज्ञ भावना के साथ मनुष्य ने अपने को जोड़ा न होता, तो अपनी शारीरिक असमर्थता और दुर्बलता के कारण अन्य पशुओं की प्रतियोगिता में यह कब का अपना अस्तित्व खो बैठा होता। यह जितना भी अब तक बढ़ा है, उसमें उसकी यज्ञ भावना ही एक मात्र माध्यम है। आगे भी यदि प्रगति करनी हो, तो उसका आधार यही भावना होगी।
प्रकृति का स्वभाव यज्ञ परंपरा के अनुरूप है। समुद्र बादलों को उदारतापूर्वक जल देता है, बादल एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे ढोकर ले जाने और बरसाने का श्रम करते हैं। नदी, नाले प्रवाहित होकर भूमि को सींचते और प्राणियों की प्यास बुझाते हैं। वृक्ष एवं वनस्पतियाँ अपने अस्तित्व का लाभ दूसरों की हो देते हैं। पुष्प और फल दूसरे के लिए ही जीते हैं। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वायु आदि की क्रियाशीलता उनके अपने लाभ के लिए नहीं, वरन् दूसरों के लिए ही है। शरीर का प्रत्येक अवयव अपने निज के लिए नहीं, वरन् समस्त शरीर के लाभ के लिए ही अनवरत गति से कार्यरत रहता है। इस प्रकार जिधर भी दृष्टिपात किया जाए, यही प्रकट होता है कि इस संसार में जो कुछ स्थिर व्यवस्था है, वह यज्ञ पर ही अवलम्बित है। यदि इसे हटा दिया जाए, तो सारे सुन्दरता कुरूपता में और सारी प्रगति विनाश में परिणत हो जायेगी। ऋषियों ने कहा है—यज्ञ ही इस संसार चक्र का धुरा है। धुरा टूट जाने पर गाड़ी का आगे बढ़ सकना कठिन है।
यज्ञीय विज्ञान
मन्त्रों में अनेक शक्ति के स्रोत दबे हैं। जिस प्रकार अमुक स्वर-विन्यास
से युक्त शब्दों की रचना करने से अनेक राग-रागिनियाँ बजती हैं और उनका
प्रभाव सुनने वालों पर विभिन्न प्रकार का होता है, उसी प्रकार
मंत्रोच्चारण से भी एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि तरंगे निकलती हैं और उनका
भारी प्रभाव विश्वव्यापी प्रकृति पर, सूक्ष्म जगत् पर तथा प्राणियों के
स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों पर पड़ता है।
यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली तत्त्व वायुमण्डल में फैलाये जाते हैं, उनसे हवा में घूमते असंख्यों रोग-कीटाणु सहज ही नष्ट होते हैं। डी.डी.टी. फिनायल आदि छिड़कने, बीमारियों से बचाव करने वाली दवाएँ या सुइयाँ लेने से भी कहीं अधिक कारगर उपाय यज्ञ करना है। साधारण रोगों एवं महामारियों से बचने का यज्ञ एक सामूहिक उपाय है। दवाओं में सीमित स्थान एवं सीमित व्यक्तियों को ही बीमारियों से बचाने की शक्ति है; पर यज्ञ की वायु तो सर्वत्र ही पहुँचती है और प्रयत्न न करने वाले प्राणियों की भी सुरक्षा करती है। मनुष्य की ही नहीं, पशु-पक्षियों, कीटाणुओं एवं वृक्ष-वनस्पतियों के आरोग्य की भी यज्ञ से रक्षा होती है।
यज्ञ की ऊष्मा मनुष्य के अंतःकरण पर देवत्व की छाप डालती है। जहाँ यज्ञ होते हैं, वह भूमि एवं प्रदेश सुसंस्कारों की छाप अपने अंदर धारण कर लेता है और वहाँ जाने वालों पर दीर्घकाल तक प्रभाव डालता रहता है। प्राचीनकाल में तीर्थ वहीं बने हैं, जहाँ बड़े-बड़े यज्ञ हुए थे। जिन घरों में, जिन स्थानों में यज्ञ होते हैं, वह भी एक प्रकार का तीर्थ बन जाता है और वहाँ जिनका आगमन रहता है, उनकी मनोभूमि उच्च, सुविकसित एवं सुसंस्कृत बनती है। महिलाएँ, छोटे बालक एवं गर्भस्थ बालक विशेष रूप से यज्ञ शक्ति से अनुप्राणित होते हैं। उन्हें सुसंस्कारी बनाने के लिए यज्ञीय वातावरण की समीपता बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है।
कुबुद्धि, कुविचार, दुर्गुण एवं दुष्कर्मों से विकृत मनोभूमि में यज्ञ से भारी सुधार होता है। इसलिए यज्ञ को पापनाशक कहा गया है। यज्ञीय प्रभाव से सुसंस्कृत हुई विवेकपूर्ण मनोभूमि का प्रतिफल जीवन के प्रत्येक क्षण को आनन्द से भर देता है, इसलिए यज्ञ को स्वर्ग देने वाला कहा गया है।
यज्ञीय धर्म प्रक्रियाओं में भाग लेने से आत्मा पर चढ़े हुए मल-विक्षेप दूर होते हैं। फलस्वरूप तेजी से उसमें ईश्वरीय प्रकाश जगता है। यज्ञ से आत्मा में ब्राह्मण-तत्त्व की वृद्धि दिनानु-दिन होती है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का परम लक्ष्य बहुत सरल हो जाता है।
यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली तत्त्व वायुमण्डल में फैलाये जाते हैं, उनसे हवा में घूमते असंख्यों रोग-कीटाणु सहज ही नष्ट होते हैं। डी.डी.टी. फिनायल आदि छिड़कने, बीमारियों से बचाव करने वाली दवाएँ या सुइयाँ लेने से भी कहीं अधिक कारगर उपाय यज्ञ करना है। साधारण रोगों एवं महामारियों से बचने का यज्ञ एक सामूहिक उपाय है। दवाओं में सीमित स्थान एवं सीमित व्यक्तियों को ही बीमारियों से बचाने की शक्ति है; पर यज्ञ की वायु तो सर्वत्र ही पहुँचती है और प्रयत्न न करने वाले प्राणियों की भी सुरक्षा करती है। मनुष्य की ही नहीं, पशु-पक्षियों, कीटाणुओं एवं वृक्ष-वनस्पतियों के आरोग्य की भी यज्ञ से रक्षा होती है।
यज्ञ की ऊष्मा मनुष्य के अंतःकरण पर देवत्व की छाप डालती है। जहाँ यज्ञ होते हैं, वह भूमि एवं प्रदेश सुसंस्कारों की छाप अपने अंदर धारण कर लेता है और वहाँ जाने वालों पर दीर्घकाल तक प्रभाव डालता रहता है। प्राचीनकाल में तीर्थ वहीं बने हैं, जहाँ बड़े-बड़े यज्ञ हुए थे। जिन घरों में, जिन स्थानों में यज्ञ होते हैं, वह भी एक प्रकार का तीर्थ बन जाता है और वहाँ जिनका आगमन रहता है, उनकी मनोभूमि उच्च, सुविकसित एवं सुसंस्कृत बनती है। महिलाएँ, छोटे बालक एवं गर्भस्थ बालक विशेष रूप से यज्ञ शक्ति से अनुप्राणित होते हैं। उन्हें सुसंस्कारी बनाने के लिए यज्ञीय वातावरण की समीपता बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है।
कुबुद्धि, कुविचार, दुर्गुण एवं दुष्कर्मों से विकृत मनोभूमि में यज्ञ से भारी सुधार होता है। इसलिए यज्ञ को पापनाशक कहा गया है। यज्ञीय प्रभाव से सुसंस्कृत हुई विवेकपूर्ण मनोभूमि का प्रतिफल जीवन के प्रत्येक क्षण को आनन्द से भर देता है, इसलिए यज्ञ को स्वर्ग देने वाला कहा गया है।
यज्ञीय धर्म प्रक्रियाओं में भाग लेने से आत्मा पर चढ़े हुए मल-विक्षेप दूर होते हैं। फलस्वरूप तेजी से उसमें ईश्वरीय प्रकाश जगता है। यज्ञ से आत्मा में ब्राह्मण-तत्त्व की वृद्धि दिनानु-दिन होती है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का परम लक्ष्य बहुत सरल हो जाता है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book