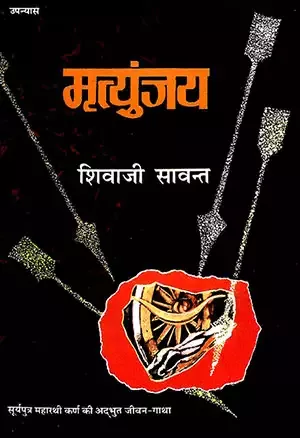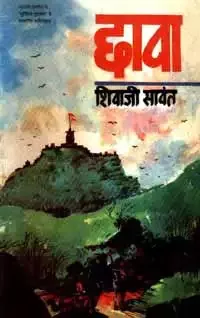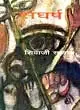|
उपन्यास >> मृत्युंजय मृत्युंजयशिवाजी सावंत
|
1045 पाठक हैं |
|||||||
महारथी दानवीर कर्ण के विराट् व्यक्तित्व पर केन्द्रित सावंत जी का यह एक अत्यन्त रोचक उपन्यास...
Mrityunjay - A Hindi Book - by Shivaji Savant
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मराठी के यशस्वी उपन्ययासकार शिवाजी सावंत का सांस्कृतिक उपन्यास मृत्युंजय आधुनिक भारतीय कथा-साहित्य में निःसन्देह एक विरल चमत्कार है। ‘मूर्तिदेवी’ पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित और अनेक भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनूदित यह कालजयी उपन्यास अपने लाखों पाठकों की सराहना पाकर इस समय भारतीय साहित्य-जगत् में लोकप्रियता के शिखर पर प्रतिष्ठित है।
मृत्युंजय उपन्यास महारथी दानवीर कर्ण के विराट् व्यक्तित्व पर केन्द्रित है। महाभारत के कई मुख्य पात्रों के बीच - जहाँ स्वयं कृष्ण भी - कर्ण की ओजस्वी, उदार, दिव्य और सर्वांगीण छवि प्रस्तुत करते हुए श्रीसावंत ने जीवन के सार्थकता, उसकी नियति और मूल-चेतना तथा मानव-सम्बन्धों की स्थिति एवं संस्कारशीलता की मार्मिक और कलात्मक अभिव्यक्ति की है।
मृत्युंजय में पौराणिक कथ्य और सनातन सांस्कृतिक चेतना के अन्तः सम्बन्धों को पूरी गरिमा के साथ उजागर किया गया है। उपन्यास को महाकाव्य का धरातल देकर चरित्र की इतनी सूक्ष्म पकड़, शैली का इतना सुन्दर निखार और भावनाओं की अभिव्यक्ति में इतना मार्मिक रसोद्रेक - सब कुछ इस उपन्यास में अनूठा है।
प्रस्तुत है मृत्युंजय का यह नवीनतम संस्करण।
मृत्युंजय उपन्यास महारथी दानवीर कर्ण के विराट् व्यक्तित्व पर केन्द्रित है। महाभारत के कई मुख्य पात्रों के बीच - जहाँ स्वयं कृष्ण भी - कर्ण की ओजस्वी, उदार, दिव्य और सर्वांगीण छवि प्रस्तुत करते हुए श्रीसावंत ने जीवन के सार्थकता, उसकी नियति और मूल-चेतना तथा मानव-सम्बन्धों की स्थिति एवं संस्कारशीलता की मार्मिक और कलात्मक अभिव्यक्ति की है।
मृत्युंजय में पौराणिक कथ्य और सनातन सांस्कृतिक चेतना के अन्तः सम्बन्धों को पूरी गरिमा के साथ उजागर किया गया है। उपन्यास को महाकाव्य का धरातल देकर चरित्र की इतनी सूक्ष्म पकड़, शैली का इतना सुन्दर निखार और भावनाओं की अभिव्यक्ति में इतना मार्मिक रसोद्रेक - सब कुछ इस उपन्यास में अनूठा है।
प्रस्तुत है मृत्युंजय का यह नवीनतम संस्करण।
आमुख
(प्रथम संस्करण से)
भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन-योजनाओं को क्रियान्वित करते समय जिस सांस्कृतिक दृष्टि को प्रमुखता दी जाती है, उसका एक अंग यह भी है कि प्राचीन और पारम्परिक कथानकों को आधुनिक-शैली शिल्प में ढालकर उनके शाश्वत मूल्य वाले पक्षों का, आज के सन्दर्भ में नवीनीकरण किया जाये। रामायण और महाभारत के संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में प्राप्त प्राचीन ग्रन्थों का प्रामाणिक सम्पादन पुराण और चरित के रूप में हुआ ही है, इधर ज्ञानपीठ ने कई ऐसे काव्य और उपन्यास प्रकाशित किये हैं जिनमें प्राचीन कथानकों की कथावस्तु को आधुनिक रूप दिया गया है।
जीवन का सतत प्रवाह काल के तटों से टकराता, उन्हें ढहाता और पुनर्निर्माण करता बहता चला आ रहा है। हर घाट की अलग छटा है, किन्तु प्रवाह का जल तात्त्विक रूप से सदा जल ही है। माटी की गन्ध, प्रकृति का परिवेश और उस परिवेश का मानवीय सृष्टि द्वारा रूपान्तर-ये सब कारण जल के रूप, रस, गन्ध, वर्ण को प्रभावित करते हैं। मानवीय भावनाओं और संवेगों की मूल प्रकृति सदा और सब कहीं एक सी है, किन्तु द्रव्य, क्षेत्र, कला परिवेश एवं मानवीय सम्पर्कों की नयी भावभूमि दृष्टि और अभिव्यक्ति के नये चमत्कार पैदा करती रहती है। तब हम राम और कृष्ण के नये रूपों का दर्शन करते हैं, हमें एक नयी उर्मिला के कोमल-करुण अन्तरंग की झाँकी मिलती है, एक नया नचिकेता और पाँच नयी द्रौपदियाँ साहित्य में अवतरित होती हैं। भारतीय ज्ञानपीठ के प्रकाशनों को ही उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करें-
जीवन का सतत प्रवाह काल के तटों से टकराता, उन्हें ढहाता और पुनर्निर्माण करता बहता चला आ रहा है। हर घाट की अलग छटा है, किन्तु प्रवाह का जल तात्त्विक रूप से सदा जल ही है। माटी की गन्ध, प्रकृति का परिवेश और उस परिवेश का मानवीय सृष्टि द्वारा रूपान्तर-ये सब कारण जल के रूप, रस, गन्ध, वर्ण को प्रभावित करते हैं। मानवीय भावनाओं और संवेगों की मूल प्रकृति सदा और सब कहीं एक सी है, किन्तु द्रव्य, क्षेत्र, कला परिवेश एवं मानवीय सम्पर्कों की नयी भावभूमि दृष्टि और अभिव्यक्ति के नये चमत्कार पैदा करती रहती है। तब हम राम और कृष्ण के नये रूपों का दर्शन करते हैं, हमें एक नयी उर्मिला के कोमल-करुण अन्तरंग की झाँकी मिलती है, एक नया नचिकेता और पाँच नयी द्रौपदियाँ साहित्य में अवतरित होती हैं। भारतीय ज्ञानपीठ के प्रकाशनों को ही उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करें-
मुक्तिदूत (उपन्यास) -वीरेन्द्र कुमार जैन
अंजना और पवनंजय का कथानक
आत्मजयी (खण्ड काव्य) -कुँवर नारायण
नचिकेता की कथा
एक और नचिकेता -गोविन्द शंकर कुरुप
मलयालम काव्य का हिन्दी अनुवाद
कनुप्रिया (खण्ड-काव्य) -धर्मवीर भारती
राधा का भाव जगत्
प्राचीना (काव्य-रूपक) -उमाशंकर जोशी
पौराणिक पात्रों का चरित्र
गुजराती से हिन्दी अनुवाद
महाश्रमण सुनें (उपन्यास) -‘भिक्खु’
व्यासपर्व (ललित निबन्ध) -दुर्गा भागवत
महाभारत के पात्रों का अध्ययन-विवेचन
मराठी से अनूदित
पूर्णावतार (उपन्यास) -प्रमथनाथ विशी
कृष्ण-कथा
बांग्ला से अनूदित
रत्नावली (खण्ड-काव्य) -हरिप्रसाद ‘हरि’
तुलसी-प्रिया का कथानक
भूमिजा (नाटक) -सर्वदानन्द
सीता की कथा-आदि-आदि।
अंजना और पवनंजय का कथानक
आत्मजयी (खण्ड काव्य) -कुँवर नारायण
नचिकेता की कथा
एक और नचिकेता -गोविन्द शंकर कुरुप
मलयालम काव्य का हिन्दी अनुवाद
कनुप्रिया (खण्ड-काव्य) -धर्मवीर भारती
राधा का भाव जगत्
प्राचीना (काव्य-रूपक) -उमाशंकर जोशी
पौराणिक पात्रों का चरित्र
गुजराती से हिन्दी अनुवाद
महाश्रमण सुनें (उपन्यास) -‘भिक्खु’
व्यासपर्व (ललित निबन्ध) -दुर्गा भागवत
महाभारत के पात्रों का अध्ययन-विवेचन
मराठी से अनूदित
पूर्णावतार (उपन्यास) -प्रमथनाथ विशी
कृष्ण-कथा
बांग्ला से अनूदित
रत्नावली (खण्ड-काव्य) -हरिप्रसाद ‘हरि’
तुलसी-प्रिया का कथानक
भूमिजा (नाटक) -सर्वदानन्द
सीता की कथा-आदि-आदि।
इसी श्रृंखला में अब यह उपन्यास ‘मृत्युंजय’। मूल उपन्यास मराठी में रचित। उपन्यासकार हैं शिवाजी सावन्त।
विचित्र है कथा इस उपन्यास-रचना की। 14 वर्ष की अवस्था में एक किशोर ने सहपाठियों के साथ एक नाटक खेला जिसमें उसने कृष्ण की भूमिका निभायी। स्कूल के मंच पर नाटक होते ही रहते हैं। नाटककार और नाटक और अभिनेता सब अपने-अपने रास्ते लगे। लेकिन इस लड़के के मन में कर्ण आकर ऐसे विराजे कि आसन से उठने का नाम ही न लें। मन की उर्वरा भूमि में सृजन का एक बीज पड़ गया। धीरे-धीरे जमीन तैयार होती रही। जब 23-24 वर्ष की आयु में शिवाजी सावन्त ने कर्ण के चरित्रों को कागज पर उतारने का प्रयत्न किया तो एक नाटक की रेखाएँ उभरकर आने लगीं, किन्तु चित्र नहीं बन पाया। और तब शिवाजी सावन्त की अन्तःप्रेरणा ने कथा-नायक को समुचित विधा की भूमिका दे दी। यह उपन्यास आकार लेने लगा। महाभारत का पारायण तो मूल आधार था ही, लेकिन दिनकर की कृति ‘रश्मिरथी’ और केदारनाथ मिश्र ‘प्रभात’ का खण्डकाव्य ‘कर्ण’ ने बीज को ऐसे सींच दिया कि अंकुर फूट आये। अंकुर फूटने से लेकर वृक्ष के पल्लवित, पुष्पित और फलित होने तक की कथा सदा ही धरा की व्यथा-कथा भी रही है और पुलक- गाथा भी।
जब 1967 में मराठी में इस उपन्यास का 3000 का प्रथम संस्करण छपा तो पाठक पढ़कर स्तब्ध रह गये। महाभारत के कई मुख्य पात्रों के बीच कर्ण को रखकर जहाँ स्वयं कृष्ण भी हैं –कर्ण की इतनी ओजस्वी, उदार, दिव्य और सर्वांगीण छवि इससे पहले अंकित ही नहीं की जा सकी थी। उपन्यास को महाकाव्य का धरातल देकर चरित्र की इतनी सूक्ष्म पकड़, शैली का इतना सुन्दर निखार और भावनाओं की अभिव्यक्ति में इतना मार्मिक रसोद्रेक अभी तक देखा नहीं गया था। कर्ण, कुन्ती, दुर्योधन, वृषाली (कर्ण-पत्नी), शोण और कृष्ण के मार्मिक आत्म-कथ्यों की श्रृंखला को रूपायित करने वाला यह उपन्यास पाठकों में इतना लोकप्रिय हुआ कि चार पाँच वर्षों में इसके चार संस्करण प्रकाशित हो चुके, प्रतियों की संख्या पचास हजार में। समीक्षकों और कृती साहित्यकारों की प्रशंसा का यह हाल कि महाराष्ट्र सरकार का साहित्य पुरस्कार इस कृति को प्राप्त हुआ; केलकर पुरस्कार, महाराष्ट्र साहित्य परिषद एवं ‘ललित’ पत्रिका पुरस्कार आदि द्वारा भी यह कृति और यह कृतिकार अभिनन्दित हुए। उपन्यास का गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। आकाशवाणी पूना से इसका रेडियों रूपान्तर भी प्रसारित हुआ है।
हिन्दी पाठकों के हाथों यह उपन्यास समर्पित करते हुए भारतीय ज्ञानपीठ को हर्ष है। इस कृति का परिचय उपन्यास के हिन्दी अनुवादक श्री ओम शिवराज के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ की सांस्कृतिक रुचि और परिष्कृत से वह प्रभावित रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। श्री शिवाजी सावन्त, श्री ओम शिवराज और भारतीय ज्ञानपीठ का त्रिविक्रम पाठकों को पुलकित करे, यह हमारी कामना है।
विचित्र है कथा इस उपन्यास-रचना की। 14 वर्ष की अवस्था में एक किशोर ने सहपाठियों के साथ एक नाटक खेला जिसमें उसने कृष्ण की भूमिका निभायी। स्कूल के मंच पर नाटक होते ही रहते हैं। नाटककार और नाटक और अभिनेता सब अपने-अपने रास्ते लगे। लेकिन इस लड़के के मन में कर्ण आकर ऐसे विराजे कि आसन से उठने का नाम ही न लें। मन की उर्वरा भूमि में सृजन का एक बीज पड़ गया। धीरे-धीरे जमीन तैयार होती रही। जब 23-24 वर्ष की आयु में शिवाजी सावन्त ने कर्ण के चरित्रों को कागज पर उतारने का प्रयत्न किया तो एक नाटक की रेखाएँ उभरकर आने लगीं, किन्तु चित्र नहीं बन पाया। और तब शिवाजी सावन्त की अन्तःप्रेरणा ने कथा-नायक को समुचित विधा की भूमिका दे दी। यह उपन्यास आकार लेने लगा। महाभारत का पारायण तो मूल आधार था ही, लेकिन दिनकर की कृति ‘रश्मिरथी’ और केदारनाथ मिश्र ‘प्रभात’ का खण्डकाव्य ‘कर्ण’ ने बीज को ऐसे सींच दिया कि अंकुर फूट आये। अंकुर फूटने से लेकर वृक्ष के पल्लवित, पुष्पित और फलित होने तक की कथा सदा ही धरा की व्यथा-कथा भी रही है और पुलक- गाथा भी।
जब 1967 में मराठी में इस उपन्यास का 3000 का प्रथम संस्करण छपा तो पाठक पढ़कर स्तब्ध रह गये। महाभारत के कई मुख्य पात्रों के बीच कर्ण को रखकर जहाँ स्वयं कृष्ण भी हैं –कर्ण की इतनी ओजस्वी, उदार, दिव्य और सर्वांगीण छवि इससे पहले अंकित ही नहीं की जा सकी थी। उपन्यास को महाकाव्य का धरातल देकर चरित्र की इतनी सूक्ष्म पकड़, शैली का इतना सुन्दर निखार और भावनाओं की अभिव्यक्ति में इतना मार्मिक रसोद्रेक अभी तक देखा नहीं गया था। कर्ण, कुन्ती, दुर्योधन, वृषाली (कर्ण-पत्नी), शोण और कृष्ण के मार्मिक आत्म-कथ्यों की श्रृंखला को रूपायित करने वाला यह उपन्यास पाठकों में इतना लोकप्रिय हुआ कि चार पाँच वर्षों में इसके चार संस्करण प्रकाशित हो चुके, प्रतियों की संख्या पचास हजार में। समीक्षकों और कृती साहित्यकारों की प्रशंसा का यह हाल कि महाराष्ट्र सरकार का साहित्य पुरस्कार इस कृति को प्राप्त हुआ; केलकर पुरस्कार, महाराष्ट्र साहित्य परिषद एवं ‘ललित’ पत्रिका पुरस्कार आदि द्वारा भी यह कृति और यह कृतिकार अभिनन्दित हुए। उपन्यास का गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। आकाशवाणी पूना से इसका रेडियों रूपान्तर भी प्रसारित हुआ है।
हिन्दी पाठकों के हाथों यह उपन्यास समर्पित करते हुए भारतीय ज्ञानपीठ को हर्ष है। इस कृति का परिचय उपन्यास के हिन्दी अनुवादक श्री ओम शिवराज के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ की सांस्कृतिक रुचि और परिष्कृत से वह प्रभावित रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। श्री शिवाजी सावन्त, श्री ओम शिवराज और भारतीय ज्ञानपीठ का त्रिविक्रम पाठकों को पुलकित करे, यह हमारी कामना है।
पृष्ठभूमि
जब-जब मैं महाभारतीय कथानायक कर्ण की जीवनी पर आधारित इस उपन्यास ‘मृत्युंजय’ का विचार करता हूँ, तब-तब अनगिनत खयाल मन में डोल उठते हैं। मराठी की यह मूल कथा। 1967 में मराठी में ख्यातनाम संस्था (कॉण्टिनेण्टल प्रकाशन’ द्वारा प्रकाशित हुई थी। उसके सात साल पहले से इस कथावस्तु की पाण्डुलिपि सिद्ध करने में जुटा रहा। मन्त्रविभोर थे वे सात साल। मैं अपना लौकिकी दैनन्दिन जीवन जैसे भूल ही गया था।
आज इस ‘मृत्युंजय’ नामक कर्णकथा के प्रेरणास्रोत का मूल ढूँढ़ने का जब मैं प्रयत्न करता हूँ तब यह संशोधन का विचार मुझे सीधे मेरी किशोरावस्था की जिन्दगी में खींच ले जाता है। उन दिनों मैं माध्यमिक शाला का छात्र था। कक्षा होगी कोई आठवीं या नौवीं। साल होगा 1956 या 57। हम-कुछ विशेष नया करना चाहने वाले छात्रों के एक ग्रुप-ने स्कूल के सम्मेलन के अवसर पर एक नाटिका का मंचन किया। उसका नाम था ‘अंगराज कर्ण’। यह नाटिका मराठी में थी। इस नाटिका में, उस किशोरावस्था में मैंने रोल किया था श्रीकृष्ण का। मुझे आज भी पूरी तरह याद है कि अपने रथ के पहिये को उखाड़ने वाले कर्ण का रोल करने वाले छात्र-मित्र ने जो संवाद किया था वह श्रीकृष्ण होकर भी मेरे हृदय को बींध गया था। कुछ-कुछ संवादांश मुझे आज भी स्मरण हैं, जैसे कि ‘‘ठहरो पार्थ, तुम क्षत्रिय हो और यह मैं रणभूमि में गड़े रथचक्र को निकाल रहा हूँ-निःशस्त्र हूँ। युद्धधर्म व राजधर्म को न भूल जाओ !’’
नाटिका खेले जाने के बहुत साल बाद भी उन कर्ण-संवादों को भूल नहीं सका था। आज ‘मृत्युंजय’ के लेखक के नाते मुझे इस कर्ण कथा का कथाबीज वह नाटिका और वह युवा कर्ण ही लगता है। मेरे सुप्त मन में ठीक अपनी जगह पकड़कर वे संवाद और वे कर्ण जमकर बैठ चुके थे।
आगे चलकर मैं अपना गाँव आजरा और अपनी शाला ‘व्यंकटराव हाईस्कूल’ छोड़कर महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए इस कलानगरी कोल्हापुर में आ गया। माध्यमिक शाला के शिक्षा-काल में ही मैंने राष्ट्रभाषा हिन्दी की कुछ परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली थीं-विशेष गुणवत्ता के साथ। खासकर उन परीक्षाओं के लिए निरन्तर अभ्यास करते रहने से हिन्दी काव्य से एक विशेष लगाव-सा हो गया था। इसलिए महाविद्यालयीन पढ़ाई में मैंने ‘हिन्दी’ भी एक विषय ले लिया। संयोग की बात है कि एफ. वॉय. बी. ए. में हिन्दी के पाठ्यक्रम में जाने-माने कविश्रेष्ठ केदारनाथ मिश्र ‘प्रभात का ‘कर्ण’ नामक खण्ड काव्य अध्ययन के लिए लिया गया।
केदारनाथ जी का यह ‘कर्ण’ खण्ड काव्य हिन्दी साहित्य जगत का एकमात्र अनमोल गहना है। केदारनाथ जी की काव्य भाषा अलंकृत होकर भी सदा सहज सुन्दर रही है। इस खण्डकाव्य में पाठक को झकझोर देने वाली कई काव्य कल्पनाएँ हैं। मैं कवि श्रेष्ठ के एक ही शब्द पर कई-कई महीनों तक विचार करता रहा। ‘कर्ण’ खण्डकाव्य के काव्यान्त में केदारनाथ जी ने बड़ी ही सहजता से दो सूक्तियाँ लिखी हैं। वे हैं-
आज इस ‘मृत्युंजय’ नामक कर्णकथा के प्रेरणास्रोत का मूल ढूँढ़ने का जब मैं प्रयत्न करता हूँ तब यह संशोधन का विचार मुझे सीधे मेरी किशोरावस्था की जिन्दगी में खींच ले जाता है। उन दिनों मैं माध्यमिक शाला का छात्र था। कक्षा होगी कोई आठवीं या नौवीं। साल होगा 1956 या 57। हम-कुछ विशेष नया करना चाहने वाले छात्रों के एक ग्रुप-ने स्कूल के सम्मेलन के अवसर पर एक नाटिका का मंचन किया। उसका नाम था ‘अंगराज कर्ण’। यह नाटिका मराठी में थी। इस नाटिका में, उस किशोरावस्था में मैंने रोल किया था श्रीकृष्ण का। मुझे आज भी पूरी तरह याद है कि अपने रथ के पहिये को उखाड़ने वाले कर्ण का रोल करने वाले छात्र-मित्र ने जो संवाद किया था वह श्रीकृष्ण होकर भी मेरे हृदय को बींध गया था। कुछ-कुछ संवादांश मुझे आज भी स्मरण हैं, जैसे कि ‘‘ठहरो पार्थ, तुम क्षत्रिय हो और यह मैं रणभूमि में गड़े रथचक्र को निकाल रहा हूँ-निःशस्त्र हूँ। युद्धधर्म व राजधर्म को न भूल जाओ !’’
नाटिका खेले जाने के बहुत साल बाद भी उन कर्ण-संवादों को भूल नहीं सका था। आज ‘मृत्युंजय’ के लेखक के नाते मुझे इस कर्ण कथा का कथाबीज वह नाटिका और वह युवा कर्ण ही लगता है। मेरे सुप्त मन में ठीक अपनी जगह पकड़कर वे संवाद और वे कर्ण जमकर बैठ चुके थे।
आगे चलकर मैं अपना गाँव आजरा और अपनी शाला ‘व्यंकटराव हाईस्कूल’ छोड़कर महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए इस कलानगरी कोल्हापुर में आ गया। माध्यमिक शाला के शिक्षा-काल में ही मैंने राष्ट्रभाषा हिन्दी की कुछ परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली थीं-विशेष गुणवत्ता के साथ। खासकर उन परीक्षाओं के लिए निरन्तर अभ्यास करते रहने से हिन्दी काव्य से एक विशेष लगाव-सा हो गया था। इसलिए महाविद्यालयीन पढ़ाई में मैंने ‘हिन्दी’ भी एक विषय ले लिया। संयोग की बात है कि एफ. वॉय. बी. ए. में हिन्दी के पाठ्यक्रम में जाने-माने कविश्रेष्ठ केदारनाथ मिश्र ‘प्रभात का ‘कर्ण’ नामक खण्ड काव्य अध्ययन के लिए लिया गया।
केदारनाथ जी का यह ‘कर्ण’ खण्ड काव्य हिन्दी साहित्य जगत का एकमात्र अनमोल गहना है। केदारनाथ जी की काव्य भाषा अलंकृत होकर भी सदा सहज सुन्दर रही है। इस खण्डकाव्य में पाठक को झकझोर देने वाली कई काव्य कल्पनाएँ हैं। मैं कवि श्रेष्ठ के एक ही शब्द पर कई-कई महीनों तक विचार करता रहा। ‘कर्ण’ खण्डकाव्य के काव्यान्त में केदारनाथ जी ने बड़ी ही सहजता से दो सूक्तियाँ लिखी हैं। वे हैं-
‘‘किन्तु कर्ण तो पहुँच चुके थे पास पिता के अपने
छोड़ तड़पते मिट्टी में मिट्टी के सारे सपने।’’
छोड़ तड़पते मिट्टी में मिट्टी के सारे सपने।’’
इन पंक्तियों में केदारनाथ जी ने खण्डकाव्य के कथानायक को सम्बोध कर ‘थे’ यह आदरवाचक क्रिया-पद दिया है। मैं उस आदरार्थी क्रिया पद पर ही थम गया। हिन्दी के प्रतिभा सम्पन्न और जाने माने इस कवि ने कर्ण के सन्दर्भ में ‘थे’ यह आदरवाचक क्रियापद क्यों लिखा होगा ? वैसे तो मूल महाभारत की संहिता में गीता प्रदान करने वाले श्रीकृष्ण को सम्बोधन करते समय एकवचनी शब्द आ चुके हैं।
इसी खण्डकाव्य में काव्यलय को प्रवाहित करने वाली कितनी ही पंक्तियाँ आयी हैं। जैसे कि,
इसी खण्डकाव्य में काव्यलय को प्रवाहित करने वाली कितनी ही पंक्तियाँ आयी हैं। जैसे कि,
‘‘दुःसाहस था कि वह
पहुँचा राजरंगशाला में-
चमके जैसा कमल चमकता
कनक किरणमाला में।’’
पहुँचा राजरंगशाला में-
चमके जैसा कमल चमकता
कनक किरणमाला में।’’
कर्ण के सुवर्ण का इतना बेजोड़ वर्णन और क्या हो सकता है ! इसलिए मैंने केदारनाथ जी का यह ‘कर्ण’ खण्डकाव्य सौ-सौ बार रटा। सुप्त मन में किशोरावस्था में सोये पड़े ‘अंगराज कर्ण’ खड़े होकर मेरे जागृतमन में छा गये थे। बार-बार मेरा अन्तर्जगत् झकझोरने लगा, ‘तुझे लिखना ही होगा-दानवीर, दिग्विजयी, अशरण, अंगराज कर्ण पर।’ पहले-पहल मन मराठी में खण्ड काव्य की ही रचना करने का हुआ। कुछ चिन्तन के उपरान्त प्रत्यक्ष आ चुका-इस सूर्यपुत्र, कुन्तिपुत्र और सार्थ अर्थ से ज्येष्ठ पाण्डव को काव्य के सीमित क्षेत्र में बाँधना कठिन है। मन फिर इसी विषय में नाटक की सोचने लगा। जल्दी ही इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि नाटक उससे भी अधूरा साहित्य प्रकार है जो इस महान् नायक को आत्मसात् कर सके। अन्त में विवरणात्मक विशाल उपन्यास लेखन के लिए मनः स्थिति दृढ़ हुई।
उपन्यास को मनःचक्षु के सामने रखकर पहले अध्ययन शुरू हुआ महाभारत का। उसमें भी अधिकतर द्रोणपर्व और कर्णपर्व पर। इस अध्ययन में मराठी के श्रेष्ठ महाभारत-भाष्यकार श्री चि. वि. वैद्य मेरे अधिक उपयुक्त मार्गदर्शक रहे। महाभारत के अधिकृत संशोधन के कारण ही वैद्यजी को मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के नाते अविरोध चुना गया था। खासकर वैद्य जी ने महाभारतीय युद्ध का कालखण्ड एक नये ढंग से निश्चित किया है। महाभारत की संहिता में जो आकाशस्थ नक्षत्रों के वर्णन आते हैं उनका सजग, गहरी दृष्टि से अध्ययन करके वैद्य जी ने यह कालखण्ड ई. पूर्व 2500 से लेकर 3000 तक निश्चित किया है। वैद्यजी का यह गम्भीर शोध मेरे लेखन-मन को और भी प्रभावित कर गया।
कर्ण के जीवन-सन्दर्भ में हिन्दी, मराठी, अँग्रेज़ी में लिखे गये नाटक, काव्य, उपन्यास, शोध पर भाष्य मैंने पढ़ने शुरू किये। साथ ही साथ, बड़ी लगन से टिप्पणियाँ लेना शुरू कर दिया। इसमें एक लक्षणीय बात मुझे नजर आयी। महाराष्ट्र व अखिल भारतवर्ष में प्रसिद्ध ‘दि केसरी’ वृत्तपत्र के सम्पादक व मराठी के जाने-माने शैलीकार श्री शि. म. परांजपे जी ने कर्ण पर मराठी में एक नाटक लिखा है। बहुत सोच-विचारकर उस नाटक का नाम उन्होंने ‘पहला पाण्डव’ रखा है। बड़े चाव से मैंने वह नाटक पढ़ा। अब अडिग, अशरण, दानवीर, दिग्विजयी, राधेय, कौन्तेय और सार्थ अर्थ में ज्येष्ठ व सर्वश्रेष्ठ वह पाण्डव मेरे लेखक मन पर पूरे-पूरे छा गये।
महाभारतीय युद्ध का समय जब नजदीक आता है तब तत्त्वज्ञान व राजकाज की अनमोल पूँजी साथ लेकर श्रीकृष्णजी शिष्टाई के लिए हस्तिनापुर आते हैं। अपना सब बुद्धिवैभव प्रण पर लगाकर समझौते का प्रस्ताव कौरवों की राज्य सभा में रखते हैं। युवराज दुर्योधन अपने गलत अभिमान से उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। महाभारतीय युद्ध अटल हो जाता है। हस्तिनापुर की राजसभा में श्रीकृष्ण वापस जाने के लिए निकलते हैं। उन्हें विदा करने के लिए आये महारथी वीरों में से वे सिर्फ कर्ण को हाथ थामकर अपने रथ पर चढ़ा लेते हैं। दोनों महावीर योद्धा राजनगर की सीमा पर एक विशाल व घने वट वृक्ष के तले पहुँचते हैं। श्रीकृष्णजी बड़े संयम से, बड़ी कुशलता से कर्ण के जन्मरहस्य का स्फोट करते हैं और अर्जुन को गीता प्रदान करने वाला अपना वही सुमधुर भाषा-वैभव फिर से प्रण पर लगाकर कर्ण को पाण्डव-पक्ष में आने के लिए आह्वान करते हैं। कर्ण मात्र अपना स्नेहभाव, दुर्योधन को दिया वचन में जगा रखते हुए अडिग रहते हैं और बड़ी नम्रता से श्रीकृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। मूल महाभारत में श्रीकृष्ण-कर्ण की इस भेंट का जो वर्णन आता है वह हृदयग्राही व बेजोड़ होने के कारण निर्लेप मन से पढ़ने लायक है।
ठीक ऐसी ही है युद्ध भूमि पर प्रस्थापित अपने शिविर से अर्घ्यदान के लिए गंगातट पर आये कर्ण-कुन्ती भेंट की घटना। समस्त विश्व के मानवीय माता-पुत्र के रिश्ते-सम्बन्ध में इतना गहरा व बेमिसाल कथाभाग अन्य किसी भाषा में नहीं है। माता-पुत्र की भेंट परस्पर सही रिश्ते जानने के बाद पहली बार होती है। उस सत्य को जानने के लिए कर्ण को लगभग पचहत्तर साल घुटते हुए राह देखनी पड़ी। महाकवि व्यास जी ने बड़ी ही रोचकता से इस भेंट की योजना लोकमाता गंगा के किनारे की है। यहाँ केवल तीन ही महान् व्यक्ति-रेखाएँ उपस्थित हैं-कर्ण, कुन्ती और गंगामाता। पूरा गंगातट निर्जन है। स्वयं व्यास जी चौथी महान् व्यक्ति-रेखा बनकर सर्वसाक्षी सवितु-सूरज के रूप में गगन में खड़े हैं। कितना लुभावना है साहित्य की भूमि पर उतरता हुआ पाठक की आँखों के सामने आने वाला यह चित्र !
इस भेंट में-पहला ही क्षणचित्र कितना आशयसम्पन्न है ! कर्ण कदम्ब वृक्ष की एक डाली पर अपना अधरीय प्रतिदिन की तरह रखकर स्नान व अर्घ्य के लिए गंगाजल में उतरते हैं। इतने में वृद्ध राजमाता कुन्ती आकर उस अधरीय की छाँव में खड़ी हो जाती हैं। कितना हृदयस्पर्शी है यह विरोधाभास ! वास्तव में माता की आँचल की छाँव में पुत्र को जीवन-धूप से बचने के लिए खड़ा होना चाहिए। यहाँ उलटा हो गया। माता ही पुत्र के वस्त्र की छाया में खड़ी है, धूप से बचने के लिए। मानो वह कर्णपिता सूर्य से मुँह छुपा रही हैं।
हर रोज की तरह, स्नान-अर्घ्यदान के बाद कर्ण ‘है कोई याचक ?’ पुकारते हुए गंगातट पर टहलते हैं। कोई भी नहीं-यह जानकर कदम्ब तले अपने अधरीय के पास आते हैं, अधरीय को डाली से खींचते हैं। उसके पीछे अपनी जन्मदात्री कुन्ती को देखकर उनका स्वाभिमान हिलोर उठता है। दोनों का निर्जन गंगातट पर, पाठक के तन पर रोंगटे खड़े करने वाला, संवाद हो जाता है। मानो दो विलक्षण सुवर्णी राजपात्र आपस में टकरा रहे हों। कर्ण अपने त्याग के लिए कुन्ती को दोषी ठहराकर उसकी निर्भर्त्सना करते हैं। कुन्ती अपनी विवशता मर्मभेदी शब्दों में बताती है। अन्त में कर्ण कुन्ती को माता के रूप में स्वीकार करते हैं। पहली बार उसे ‘माँ’ कहकर पुकारते हैं।
प्रारम्भ में संघर्ष से शुरू हुआ यह कथाभाग अन्त में पाठक का हृदय हिलाकर समाप्त हो जाता है। यह ‘कर्ण-कुन्ती’ भेंट व इसके पहले घटी ‘श्रीकृष्ण-कर्ण भेंट’ एक लेखक के नाते मुझे चुनौती-सी लगी। इन दोनों घटनाओं में, मूल महाभारतीय संहिता में रह गयी कुछ त्रुटियाँ मुझे महसूस होने लगीं, बेचैन करने लगीं। कई दिनों तक मैंने इस पर चिन्तन किया। कर्ण-कुन्ती-श्रीकृष्ण इन व्यक्तिरेखाओं ने मुझे रात-दिन घेर रखा। अकथनीय ढंग से वे मुझे सताने लगे।
एक दिन स्नानादि दैनिक कर्म करने के बाद मैं पूजा करने बैठा। भावपूर्ण मन से मैंने ‘ओम् भूर्भुवः स्वः’-इस सवितु मन्त्र का उच्चारण किया। ठानकर लिखने बैठा। आत्मनिवेदनपरक शैली का मुझे ही-चौंकानेवाला आविष्करण आप ही आप होने लगा। पहले ही प्रकरण में कर्ण बोलने लगे-‘आज मुझे अपनी कहानी सबको सुनानी है।’ बस्स, मैं लिखता ही चला गया। पहला प्रकरण पूर्ण हुआ। अवर्णनीय आनन्द की लहरों से मेरा मन भर उठा। निर्मिति का आनन्द केवल कलाकार ही जान सकते हैं। झट ही दूसरा प्रकरण-कर्ण को पालने वाले अधिरथ व राधा के पुत्र ‘शोण’ के आत्मनिवेदन से पूर्ण हुआ। वे दिन मन्त्रभारति थे। सृजन का काल कला-जगत् में हमेशा ही मन्त्रभारित रहता है।
इन दो प्रकरणों के बाद मुझे तीव्रता से महसूस होने लगा कि ‘भाई, यह कोई ठीक बात नहीं। जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह महासंग्राम हुआ, उस कथाविषय को जिन्दा करने वाली भूमि देखे बिना लिखना निरा झूठापन है।’ मुझे कुरुक्षेत्र व इर्द-गिर्द का परिसर आँखों से देखना ही होगा। अब मन इसी बात पर अड़ गया।
उन दिनों मैं कोल्हापुर के राजाराम हाईस्कूल में माध्यमिक शिक्षक के नाते सेवा करता था। सबसे पहले सवाल था सैर के जरूरी दो-तीन महीनों की छुट्टी का। उसके बाद सवाल था सैर के लिए आवश्यक पैसों का। हर तरह की कोशिश के बाद मैंने इन समस्याओं को हल किया। और एक शुभ दिन मैं अकेला ही निकला कोल्हापुर से कुरुक्षेत्र तक सैर करने के लिए। साथ में था एक अच्छे लेन्स वाला कैंमरा। और मन में थी कुरुक्षेत्र भूमि पैदल ही घूमने की अदम्य इच्छा, मैं केवल इतना ही जानता था कि कुरुक्षेत्र भूमि दिल्ली के कहीं आसपास है। कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री बुद्धप्रकाश जी से मैंने पत्रव्यवहार किया। उनका सानन्द जवाब आया ‘अवश्य आ जाइये। जरूर सहायता मिलेगी।’
मैं जब दिल्ली पहुँचा तब जाड़े के दिन थे। वह 1965 का अक्तूबर का महीना था। करोलबाग में स्थित ‘पूना गेस्ट हाउस’ में अपना सामान रखकर मैं दिल्ली से कुरुक्षेत्र जा पहुँचा। कुरुक्षेत्र के ‘गीता हाईस्कूल’ के प्रमुख अध्यापक श्री विश्वनाथ जी के घर उनके परिवार का ही एक सदस्य बनकर मैं रहा। अब मेरा कुरुक्षेत्र पर्यटन शुरू हुआ। हर रोज बड़े सवेरे छः बजे उठकर मैं स्नान-नाश्ता करने के बाद पैदल ही चल पड़ता। सबसे पहले मैंने देखा वह स्थान जिसे ‘कर्ण का टीला’ कहते हैं। यह स्थल महाभारतीय युद्ध में सेनापति कर्ण का सेना पर नजर रखने के लिए महात्वपूर्ण स्थान था। उस टीले पर मैं आधा घण्टा तक आँखें भींचे घास पर लेटा रहा। वहाँ से बहने वाले मन्द वायु के झोंके मुझसे अबोध बातें कर रहे थे। वह अनुभूति अवर्णनीय थी।
सैर का दूसरा चरण शुरू हुआ। अब मैंने कुरुक्षेत्र पर स्थित जलपूर्ण सरोवर एक के बाद एक देखे। पहले देखा ‘सूर्य सरोवर’। इस सरोवर का वर्णन महाभारत में आता है। उसके बाद ‘ज्योति सर’ यानी ‘ज्योति सरोवर’। यह वह स्थान है जहाँ पर श्रीकृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का हितोपदेश दिया था। आज वहाँ पर संगमर्मर का रथ और उसमें स्थित अर्जुन को उपदेश देने वाले श्रीकृष्ण जी की मूर्ति है। संगमर्मर का एक गीता-मन्दिर भी है। इसके बाद सुयोग आया नदी दृशद्वती देखने का। यह वह नदी है जिसमें युधिष्ठिर ने युद्ध में हत सभी योद्धाओं के लिए तर्पण दिया था। श्रीकृष्ण जी के कहने से पहला तर्पण कर्ण को दिया गया था।
अब सैर का तीसरा चरण आ गया। जहाँ कर्ण के रथ का पहिया युद्धभूमि में फँस गया था, वह ‘अमीन पहाड़ी’ मैं देख रहा था। मेरे मन में कई सम्मिश्र भावनाओं की खलबली मची हुई थी।
इसके बाद मैं हरियाणा में उतरा। कर्ण के नाम पर मशहूर ‘करनाल’ नामक शहर देखा। वहाँ से मैं मेरठ के नजदीक सदियों से विख्यात हस्तिनापुर आ गया। वहाँ आज भी कर्ण की निशानी बताने वाला एक कर्ण-मन्दिर है। समस्त भारतवर्ष में शायद यह एक ही मन्दिर होगा जिसमें किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं है। उस मन्दिर के स्थान पर खड़ा रहकर कर्ण याचकों को दान दिया करते थे। इस स्थान पर मैं विचारों में खोया खड़ा रहा। इसी जगह पर कवच-कुण्डल-दान की विश्वविख्यात घटना घटी थी।
यहाँ से मैं दिल्ली वापस लौटा, जो कभी ‘इन्द्रप्रस्थ’ थी। यहाँ मैंने पाण्डव-बावड़ी नाम की जगह देखी।
वापस लौटते समय मैंने मथुरा, श्रीकृष्ण का जन्मस्थल, वृन्दावन-गोवर्धन व गोकुल देखा। बाणों से ठसाठस भरे हुए तरकस की तरह विचार मन में लेकर मैं कोल्हापुर लौटा। अब मुझसे लिखे बिना रहना मुश्किल था। एक के बाद एक प्रकरण सिद्ध होने लगे। जैसे कि दुर्योधन, कुन्ती, फिर से कर्ण-शोण व सरताज जैसा अन्तिम प्रकरण-श्रीकृष्ण। मुझे यह आग्रह से कहना है कि महाभारत न केवल पुराण-कथा है बल्कि इस भारतवर्ष का प्रागैतिहासिक काल का सबसे पुराना उपलब्ध इतिहास है।
कर्ण के समस्त जीवन को स्पर्श करने वाला उपन्यास ‘मृत्युंजय’ सिद्ध हो गया। यह पाण्डुलिपि अठारह सौ पृष्ठों की बन गयी। सौभाग्यवश इस उपन्यास को मराठी के ’कॉण्टिनेण्टल प्रकाशन’ के अनुभवी प्रकाशक श्री अनन्तरावजी कुलकर्णी मिल गये। साथ-साथ विख्यात चित्रकार श्री दीनानाथ जी दलाल सजावट के लिए प्राप्त हो गये। 1967 में गणेश-जन्म के शुभ अवसर पर मराठी के महाकवि गजानन माडगुलकरजी के मांगलिक हाथों से प्रकाशन हुआ ! मराठी व हिन्दी पाठकों ने इस कर्णकथा ‘मृत्युंजय’ का खुले दिल से स्वागत किया। ‘मृत्युंजय’ अब मेरा नहीं रहा, वह समस्त पाठकों का हो चुका है। भारतीय ज्ञानपीठ के रत्नपारखी संचालक श्रीमान लक्ष्मीचन्द्र जैन ने मृत्युंजय का 1974 में हिन्दी अनुवाद कराया, अनुवाद के इस कार्य को माण्ट (मथुरा) के एस. व्ही. ए. कॉलेज के प्राध्यापक श्री ओम शिवराज जी ने बड़ी सामर्थ्य से निभाया है सन् 1975 में ही प्रथम प्रयोग से मराठी रंगमंच पर खेला गया इसी नाम का नाटक आज भी खेला जा रहा है।
मैं अब भी जब मृत्युंजय का विचार करता हूँ, मुझे तीव्रता से लगता है कि यह सारे जग को उजाला देने वाले प्रकाश के स्वामी सवितु यानी सूर्यदेव की ही इच्छा थी। बड़ी नम्रता से मैं हमेशा कहता आया और कहता रहूँगा कि मैं बस एक निमित्तमात्र हूँ।
आज इस नये संस्करण के प्रकाशन के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी पाठकों की ओर से एवं व्यक्तिगत श्रद्धाभाव से यह नूतन ‘अर्घ्यदान’ उस अशरण, महादानी सूर्यपुत्र ‘कर्ण’ के ही चरणों में अर्पित करता हूँ।
उपन्यास को मनःचक्षु के सामने रखकर पहले अध्ययन शुरू हुआ महाभारत का। उसमें भी अधिकतर द्रोणपर्व और कर्णपर्व पर। इस अध्ययन में मराठी के श्रेष्ठ महाभारत-भाष्यकार श्री चि. वि. वैद्य मेरे अधिक उपयुक्त मार्गदर्शक रहे। महाभारत के अधिकृत संशोधन के कारण ही वैद्यजी को मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के नाते अविरोध चुना गया था। खासकर वैद्य जी ने महाभारतीय युद्ध का कालखण्ड एक नये ढंग से निश्चित किया है। महाभारत की संहिता में जो आकाशस्थ नक्षत्रों के वर्णन आते हैं उनका सजग, गहरी दृष्टि से अध्ययन करके वैद्य जी ने यह कालखण्ड ई. पूर्व 2500 से लेकर 3000 तक निश्चित किया है। वैद्यजी का यह गम्भीर शोध मेरे लेखन-मन को और भी प्रभावित कर गया।
कर्ण के जीवन-सन्दर्भ में हिन्दी, मराठी, अँग्रेज़ी में लिखे गये नाटक, काव्य, उपन्यास, शोध पर भाष्य मैंने पढ़ने शुरू किये। साथ ही साथ, बड़ी लगन से टिप्पणियाँ लेना शुरू कर दिया। इसमें एक लक्षणीय बात मुझे नजर आयी। महाराष्ट्र व अखिल भारतवर्ष में प्रसिद्ध ‘दि केसरी’ वृत्तपत्र के सम्पादक व मराठी के जाने-माने शैलीकार श्री शि. म. परांजपे जी ने कर्ण पर मराठी में एक नाटक लिखा है। बहुत सोच-विचारकर उस नाटक का नाम उन्होंने ‘पहला पाण्डव’ रखा है। बड़े चाव से मैंने वह नाटक पढ़ा। अब अडिग, अशरण, दानवीर, दिग्विजयी, राधेय, कौन्तेय और सार्थ अर्थ में ज्येष्ठ व सर्वश्रेष्ठ वह पाण्डव मेरे लेखक मन पर पूरे-पूरे छा गये।
महाभारतीय युद्ध का समय जब नजदीक आता है तब तत्त्वज्ञान व राजकाज की अनमोल पूँजी साथ लेकर श्रीकृष्णजी शिष्टाई के लिए हस्तिनापुर आते हैं। अपना सब बुद्धिवैभव प्रण पर लगाकर समझौते का प्रस्ताव कौरवों की राज्य सभा में रखते हैं। युवराज दुर्योधन अपने गलत अभिमान से उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। महाभारतीय युद्ध अटल हो जाता है। हस्तिनापुर की राजसभा में श्रीकृष्ण वापस जाने के लिए निकलते हैं। उन्हें विदा करने के लिए आये महारथी वीरों में से वे सिर्फ कर्ण को हाथ थामकर अपने रथ पर चढ़ा लेते हैं। दोनों महावीर योद्धा राजनगर की सीमा पर एक विशाल व घने वट वृक्ष के तले पहुँचते हैं। श्रीकृष्णजी बड़े संयम से, बड़ी कुशलता से कर्ण के जन्मरहस्य का स्फोट करते हैं और अर्जुन को गीता प्रदान करने वाला अपना वही सुमधुर भाषा-वैभव फिर से प्रण पर लगाकर कर्ण को पाण्डव-पक्ष में आने के लिए आह्वान करते हैं। कर्ण मात्र अपना स्नेहभाव, दुर्योधन को दिया वचन में जगा रखते हुए अडिग रहते हैं और बड़ी नम्रता से श्रीकृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। मूल महाभारत में श्रीकृष्ण-कर्ण की इस भेंट का जो वर्णन आता है वह हृदयग्राही व बेजोड़ होने के कारण निर्लेप मन से पढ़ने लायक है।
ठीक ऐसी ही है युद्ध भूमि पर प्रस्थापित अपने शिविर से अर्घ्यदान के लिए गंगातट पर आये कर्ण-कुन्ती भेंट की घटना। समस्त विश्व के मानवीय माता-पुत्र के रिश्ते-सम्बन्ध में इतना गहरा व बेमिसाल कथाभाग अन्य किसी भाषा में नहीं है। माता-पुत्र की भेंट परस्पर सही रिश्ते जानने के बाद पहली बार होती है। उस सत्य को जानने के लिए कर्ण को लगभग पचहत्तर साल घुटते हुए राह देखनी पड़ी। महाकवि व्यास जी ने बड़ी ही रोचकता से इस भेंट की योजना लोकमाता गंगा के किनारे की है। यहाँ केवल तीन ही महान् व्यक्ति-रेखाएँ उपस्थित हैं-कर्ण, कुन्ती और गंगामाता। पूरा गंगातट निर्जन है। स्वयं व्यास जी चौथी महान् व्यक्ति-रेखा बनकर सर्वसाक्षी सवितु-सूरज के रूप में गगन में खड़े हैं। कितना लुभावना है साहित्य की भूमि पर उतरता हुआ पाठक की आँखों के सामने आने वाला यह चित्र !
इस भेंट में-पहला ही क्षणचित्र कितना आशयसम्पन्न है ! कर्ण कदम्ब वृक्ष की एक डाली पर अपना अधरीय प्रतिदिन की तरह रखकर स्नान व अर्घ्य के लिए गंगाजल में उतरते हैं। इतने में वृद्ध राजमाता कुन्ती आकर उस अधरीय की छाँव में खड़ी हो जाती हैं। कितना हृदयस्पर्शी है यह विरोधाभास ! वास्तव में माता की आँचल की छाँव में पुत्र को जीवन-धूप से बचने के लिए खड़ा होना चाहिए। यहाँ उलटा हो गया। माता ही पुत्र के वस्त्र की छाया में खड़ी है, धूप से बचने के लिए। मानो वह कर्णपिता सूर्य से मुँह छुपा रही हैं।
हर रोज की तरह, स्नान-अर्घ्यदान के बाद कर्ण ‘है कोई याचक ?’ पुकारते हुए गंगातट पर टहलते हैं। कोई भी नहीं-यह जानकर कदम्ब तले अपने अधरीय के पास आते हैं, अधरीय को डाली से खींचते हैं। उसके पीछे अपनी जन्मदात्री कुन्ती को देखकर उनका स्वाभिमान हिलोर उठता है। दोनों का निर्जन गंगातट पर, पाठक के तन पर रोंगटे खड़े करने वाला, संवाद हो जाता है। मानो दो विलक्षण सुवर्णी राजपात्र आपस में टकरा रहे हों। कर्ण अपने त्याग के लिए कुन्ती को दोषी ठहराकर उसकी निर्भर्त्सना करते हैं। कुन्ती अपनी विवशता मर्मभेदी शब्दों में बताती है। अन्त में कर्ण कुन्ती को माता के रूप में स्वीकार करते हैं। पहली बार उसे ‘माँ’ कहकर पुकारते हैं।
प्रारम्भ में संघर्ष से शुरू हुआ यह कथाभाग अन्त में पाठक का हृदय हिलाकर समाप्त हो जाता है। यह ‘कर्ण-कुन्ती’ भेंट व इसके पहले घटी ‘श्रीकृष्ण-कर्ण भेंट’ एक लेखक के नाते मुझे चुनौती-सी लगी। इन दोनों घटनाओं में, मूल महाभारतीय संहिता में रह गयी कुछ त्रुटियाँ मुझे महसूस होने लगीं, बेचैन करने लगीं। कई दिनों तक मैंने इस पर चिन्तन किया। कर्ण-कुन्ती-श्रीकृष्ण इन व्यक्तिरेखाओं ने मुझे रात-दिन घेर रखा। अकथनीय ढंग से वे मुझे सताने लगे।
एक दिन स्नानादि दैनिक कर्म करने के बाद मैं पूजा करने बैठा। भावपूर्ण मन से मैंने ‘ओम् भूर्भुवः स्वः’-इस सवितु मन्त्र का उच्चारण किया। ठानकर लिखने बैठा। आत्मनिवेदनपरक शैली का मुझे ही-चौंकानेवाला आविष्करण आप ही आप होने लगा। पहले ही प्रकरण में कर्ण बोलने लगे-‘आज मुझे अपनी कहानी सबको सुनानी है।’ बस्स, मैं लिखता ही चला गया। पहला प्रकरण पूर्ण हुआ। अवर्णनीय आनन्द की लहरों से मेरा मन भर उठा। निर्मिति का आनन्द केवल कलाकार ही जान सकते हैं। झट ही दूसरा प्रकरण-कर्ण को पालने वाले अधिरथ व राधा के पुत्र ‘शोण’ के आत्मनिवेदन से पूर्ण हुआ। वे दिन मन्त्रभारति थे। सृजन का काल कला-जगत् में हमेशा ही मन्त्रभारित रहता है।
इन दो प्रकरणों के बाद मुझे तीव्रता से महसूस होने लगा कि ‘भाई, यह कोई ठीक बात नहीं। जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह महासंग्राम हुआ, उस कथाविषय को जिन्दा करने वाली भूमि देखे बिना लिखना निरा झूठापन है।’ मुझे कुरुक्षेत्र व इर्द-गिर्द का परिसर आँखों से देखना ही होगा। अब मन इसी बात पर अड़ गया।
उन दिनों मैं कोल्हापुर के राजाराम हाईस्कूल में माध्यमिक शिक्षक के नाते सेवा करता था। सबसे पहले सवाल था सैर के जरूरी दो-तीन महीनों की छुट्टी का। उसके बाद सवाल था सैर के लिए आवश्यक पैसों का। हर तरह की कोशिश के बाद मैंने इन समस्याओं को हल किया। और एक शुभ दिन मैं अकेला ही निकला कोल्हापुर से कुरुक्षेत्र तक सैर करने के लिए। साथ में था एक अच्छे लेन्स वाला कैंमरा। और मन में थी कुरुक्षेत्र भूमि पैदल ही घूमने की अदम्य इच्छा, मैं केवल इतना ही जानता था कि कुरुक्षेत्र भूमि दिल्ली के कहीं आसपास है। कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री बुद्धप्रकाश जी से मैंने पत्रव्यवहार किया। उनका सानन्द जवाब आया ‘अवश्य आ जाइये। जरूर सहायता मिलेगी।’
मैं जब दिल्ली पहुँचा तब जाड़े के दिन थे। वह 1965 का अक्तूबर का महीना था। करोलबाग में स्थित ‘पूना गेस्ट हाउस’ में अपना सामान रखकर मैं दिल्ली से कुरुक्षेत्र जा पहुँचा। कुरुक्षेत्र के ‘गीता हाईस्कूल’ के प्रमुख अध्यापक श्री विश्वनाथ जी के घर उनके परिवार का ही एक सदस्य बनकर मैं रहा। अब मेरा कुरुक्षेत्र पर्यटन शुरू हुआ। हर रोज बड़े सवेरे छः बजे उठकर मैं स्नान-नाश्ता करने के बाद पैदल ही चल पड़ता। सबसे पहले मैंने देखा वह स्थान जिसे ‘कर्ण का टीला’ कहते हैं। यह स्थल महाभारतीय युद्ध में सेनापति कर्ण का सेना पर नजर रखने के लिए महात्वपूर्ण स्थान था। उस टीले पर मैं आधा घण्टा तक आँखें भींचे घास पर लेटा रहा। वहाँ से बहने वाले मन्द वायु के झोंके मुझसे अबोध बातें कर रहे थे। वह अनुभूति अवर्णनीय थी।
सैर का दूसरा चरण शुरू हुआ। अब मैंने कुरुक्षेत्र पर स्थित जलपूर्ण सरोवर एक के बाद एक देखे। पहले देखा ‘सूर्य सरोवर’। इस सरोवर का वर्णन महाभारत में आता है। उसके बाद ‘ज्योति सर’ यानी ‘ज्योति सरोवर’। यह वह स्थान है जहाँ पर श्रीकृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का हितोपदेश दिया था। आज वहाँ पर संगमर्मर का रथ और उसमें स्थित अर्जुन को उपदेश देने वाले श्रीकृष्ण जी की मूर्ति है। संगमर्मर का एक गीता-मन्दिर भी है। इसके बाद सुयोग आया नदी दृशद्वती देखने का। यह वह नदी है जिसमें युधिष्ठिर ने युद्ध में हत सभी योद्धाओं के लिए तर्पण दिया था। श्रीकृष्ण जी के कहने से पहला तर्पण कर्ण को दिया गया था।
अब सैर का तीसरा चरण आ गया। जहाँ कर्ण के रथ का पहिया युद्धभूमि में फँस गया था, वह ‘अमीन पहाड़ी’ मैं देख रहा था। मेरे मन में कई सम्मिश्र भावनाओं की खलबली मची हुई थी।
इसके बाद मैं हरियाणा में उतरा। कर्ण के नाम पर मशहूर ‘करनाल’ नामक शहर देखा। वहाँ से मैं मेरठ के नजदीक सदियों से विख्यात हस्तिनापुर आ गया। वहाँ आज भी कर्ण की निशानी बताने वाला एक कर्ण-मन्दिर है। समस्त भारतवर्ष में शायद यह एक ही मन्दिर होगा जिसमें किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं है। उस मन्दिर के स्थान पर खड़ा रहकर कर्ण याचकों को दान दिया करते थे। इस स्थान पर मैं विचारों में खोया खड़ा रहा। इसी जगह पर कवच-कुण्डल-दान की विश्वविख्यात घटना घटी थी।
यहाँ से मैं दिल्ली वापस लौटा, जो कभी ‘इन्द्रप्रस्थ’ थी। यहाँ मैंने पाण्डव-बावड़ी नाम की जगह देखी।
वापस लौटते समय मैंने मथुरा, श्रीकृष्ण का जन्मस्थल, वृन्दावन-गोवर्धन व गोकुल देखा। बाणों से ठसाठस भरे हुए तरकस की तरह विचार मन में लेकर मैं कोल्हापुर लौटा। अब मुझसे लिखे बिना रहना मुश्किल था। एक के बाद एक प्रकरण सिद्ध होने लगे। जैसे कि दुर्योधन, कुन्ती, फिर से कर्ण-शोण व सरताज जैसा अन्तिम प्रकरण-श्रीकृष्ण। मुझे यह आग्रह से कहना है कि महाभारत न केवल पुराण-कथा है बल्कि इस भारतवर्ष का प्रागैतिहासिक काल का सबसे पुराना उपलब्ध इतिहास है।
कर्ण के समस्त जीवन को स्पर्श करने वाला उपन्यास ‘मृत्युंजय’ सिद्ध हो गया। यह पाण्डुलिपि अठारह सौ पृष्ठों की बन गयी। सौभाग्यवश इस उपन्यास को मराठी के ’कॉण्टिनेण्टल प्रकाशन’ के अनुभवी प्रकाशक श्री अनन्तरावजी कुलकर्णी मिल गये। साथ-साथ विख्यात चित्रकार श्री दीनानाथ जी दलाल सजावट के लिए प्राप्त हो गये। 1967 में गणेश-जन्म के शुभ अवसर पर मराठी के महाकवि गजानन माडगुलकरजी के मांगलिक हाथों से प्रकाशन हुआ ! मराठी व हिन्दी पाठकों ने इस कर्णकथा ‘मृत्युंजय’ का खुले दिल से स्वागत किया। ‘मृत्युंजय’ अब मेरा नहीं रहा, वह समस्त पाठकों का हो चुका है। भारतीय ज्ञानपीठ के रत्नपारखी संचालक श्रीमान लक्ष्मीचन्द्र जैन ने मृत्युंजय का 1974 में हिन्दी अनुवाद कराया, अनुवाद के इस कार्य को माण्ट (मथुरा) के एस. व्ही. ए. कॉलेज के प्राध्यापक श्री ओम शिवराज जी ने बड़ी सामर्थ्य से निभाया है सन् 1975 में ही प्रथम प्रयोग से मराठी रंगमंच पर खेला गया इसी नाम का नाटक आज भी खेला जा रहा है।
मैं अब भी जब मृत्युंजय का विचार करता हूँ, मुझे तीव्रता से लगता है कि यह सारे जग को उजाला देने वाले प्रकाश के स्वामी सवितु यानी सूर्यदेव की ही इच्छा थी। बड़ी नम्रता से मैं हमेशा कहता आया और कहता रहूँगा कि मैं बस एक निमित्तमात्र हूँ।
आज इस नये संस्करण के प्रकाशन के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी पाठकों की ओर से एवं व्यक्तिगत श्रद्धाभाव से यह नूतन ‘अर्घ्यदान’ उस अशरण, महादानी सूर्यपुत्र ‘कर्ण’ के ही चरणों में अर्पित करता हूँ।
-शिवाजी सावन्त
कर्ण
आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ ! मेरी बात को सुनकर कुछ लोग चौंकेंगे ! कहेंगे, जो काल के मुख में जा चुके, वे कैसे बोलने लगे ? लेकिन एक समय ऐसा भी आता है, जब ऐसे लोगों को भी बोलना पड़ता है ! जब-जब हाड़-मांस के जीवित पुतले मृतकों की तरह आचरण करने लगते हैं, तब-तब मृतकों को जीवित होकर बोलना ही पड़ता है ! आह, आज मैं औरों के लिए कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस तरह की बात करने वाला मैं कोई बहुत बड़ा दार्शनिक नहीं हूँ। संसार मेरे सामने एक युद्ध-क्षेत्र के रूप में ही उपस्थित हुआ ! और मेरा जीवन भी क्या है ! उस युद्ध-क्षेत्र में बाणों का केवल एक तरकश ! अनेक प्रकार की, अनेक आकारों की विविध घटनाओं के बाण जिसमें ठसाठस भरे हुए हैं-बस ऐसा ही केवल एक तरकश !!
आज अपने जीवन के उस तरकश को मैं सबके सामने अच्छी तरह खोलकर दिखा देना चाहता हूँ ! उसमें रखे हुए विविध घटनाओं के बाणों को-बिल्कुल एक-सी सभी घटनाओं के बाणों को-मैं मुक्त मन से अपने ही हाथों से सबको दिखा देना चाहता हूँ। अपने दिव्य फलकों से चमचमाते हुए, अपने पौरुष और आकर्षक आकार के कारण तत्क्षण मन को मोह लेने वाले, साथ ही टूटे हुए पुच्छ के कारण दयनीय दिखाई देने वाले तथा जहाँ-तहाँ टूटे हुए फलकों के कारण अटपटे और अजीब-से प्रतीत होने वाले सभी बाणों को-और वे भी जैसे हैं वैसे ही-मैं आज सबको दिखाना चाहता हूँ !
विश्व की श्रेष्ठ वीरता की तुला पर मैं उनकी अच्छी तरह परख कराना चाहता हूँ। धरणीतल के समस्त मातृत्व के द्वारा आज मैं उनका वास्तविक मूल्य निश्चित कराना चाहता हूँ। पृथ्वीतल के एक-एक की गुरुता द्वारा मैं उनका वास्तविक स्थान निर्धारित कराना चाहता हूँ। प्राणों की बाज़ी लगा देने वाली मित्रता के द्वारा मैं आज उनकी परीक्षा कराना चाहता हूँ। हार्दिक फुहारों से भीग जानेवाले बन्धुत्व के द्वारा मैं उनका वास्तविक मूल्यांकन कराना चाहता हूँ।
भीतर से-मेरे मन के एकदम गहन-गम्भीर अन्तरतम से एक आवाज बार-बार मुझको सुनाई देने लगी है। दृढ़ निश्चय के साथ जैसे-जैसे मैं मन ही मन उस आवाज़ को रोकने का प्रयत्न करता हूँ, वैसे-ही-वैसे हवा के तीव्र झोंको से अग्नि की ज्वाला जैसे बुझने के बजाय पहले की अपेक्षा और अधिक जोर से भड़क उठती है, वैसे ही वह आवाज बार-बार गरजकर मुझसे कहती है, ‘‘कहो कर्ण ! अपनी जीवन कथा आज सबको बता दो। वह कथा तुम ऐसी भाषा में कहो कि सब समझ सकें, क्योंकि आज परिस्थिति ही ऐसी है। सारा संसार कह रहा है, ‘कर्ण, तेरा जीवन तो चिथड़े के समान था !’ कहो, गरजकर सबसे कहो कि वह चिथड़ा नहीं था, बल्कि वह तो गोटा किनारवाला एक अतलसी राजवस्त्र था। केवल-परिस्थितियों के निर्दय कँटीले बाड़े में उलझने से ही उसके सहस्त्रों चिथड़े हो गये थे। जिस किसी के हाथ में वे पड़े, उसने मनमाने ढंग से उनका प्रचार किया। और फिर भी तुमको उस राजवस्त्र पर इतना अभिमान क्यों ?’’
वस्तुओं के किसी ढेर में सुन्दर सन्दूक की तह में पड़े हुए नये निकोर और अखण्ड राजवस्त्र की अपेक्षा, भयंकर ताण्डव करने वाले काल के झंझावात से अकेले जूझते हुए चीर-चीर होने वाला यह तेरा राजवस्त्र क्या कम मूल्यवान् था, यह आज सबको आँखें खोलकर अच्छी तरह देख लेने दे ! कान खोलकर अच्छी तरह सुन लेने दे ! वीरों की कहानियाँ सदैव ही बड़ी रुचि से सुननेवाले तथा दूसरे ही क्षण-एकदम दूसरे ही क्षण उतनी ही सरलता और निश्चिन्तता से बिलकुल ही भूल जानेवाले इस पागल संसार को तेरी यह कहानी क्या कभी ज़ोर से झकझोर सकेगी ? क्या उसमें इतनी प्रचण्ड शक्ति है ?
विश्व की चरम सत्यता पर जिनका अखण्ड विश्वास है, जो लोग मृत्यु को एक खिलौना समझते है, सिंह की-सी छाती वाले जिन वीरों का इस धराधाम पर अस्तित्व है, वे सभी लोग आज तुम्हारी कहानी को सुनना चाहेंगे। आह ! यह क्या केवल कहानी है ? यह तो एक महान् सत्य है। और सत्य देखने वालों की और सुनने वालों की इच्छा का विचार कभी नहीं किया जाता। वह सदैव जिसरूप में होता है, उसी रूप में सामने आया करता है उदित होते हुए सूर्यदेव की तरह।
कथा कोई भी हो, उसको सुनते समय श्रोता यह आशा करते हैं कि उसमें मदिरा के मधुर चषक होंगे ! नर्तकियों का नादमय पदन्यास होंगे और होंगे स्त्री-पुरुष के आवेग पूर्ण आलिंगन ! वे उसमें एक ऐसा नशा चाहते हैं जो क्षणभंगुर जीवन की प्रतीति को एकदम भुला दे। जो कहानी मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी उस जीवन गाथा में मदिरा के ऐसे चषक नहीं है। मन को धीरे से गुदगुदाने वाले नर्तकियों के पदन्यास भी नहीं है उसमें है केवल संग्राम। भिन्न-भिन्न प्रकार के भावों को कँपा देने वाला संग्राम !
मैं तो तन-मन से लड़ने वाला केवल एक असभ्य सैनिक हूँ। मैं अपनी कहानी आज अपने केवल अपने ही समाधान के लिए कह रहा हूँ। मनुष्य अपने मन की बात जब तक कहीं कह नहीं लेता, तब तक उसका मन हलका ही नहीं होता। इसलिए मैं अपनी यह कहानी मुक्त मन से कहने जा रहा हूँ।
लेकिन अब मेरे सामने वास्तविक कठिनाई तो यह है कि अपनी इस संग्राम-कथा को मैं काल-क्रमानुसार कैसे कहूँ ? क्योंकि, कड़कड़ाती हुई बिजली की कानों के परदे फाड़ डालने वाली मर्मभेदी आवाज़ सुनकर वन्य घोड़ों के झुण्ड के अनेक घोड़े जैसे जिधर रास्ता मिलता है, उधर ही दौड़ने लगते हैं; वैसे ही अनेक घटनाएँ इस समय मेरी आँखों के सामने कालक्रम को छोड़कर इधर-उधर मनचाही दौड़ लगा रही हैं उनको कालक्रमानुसार कैसे जोड़ूँ, यह स्वयं मुझे भी नहीं सूझ रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस समय बार-बार मेरी आँखों के सामने जो खड़ी हो रही है, वह है गंगामाता के पवित्र और रमणीय तीर पर बसी हुई चम्पानगरी। चम्पानगरी मेरी जीवन सरिता का वह सुन्दर मोड़ है, जो मुझको ही प्रिय लगता है।
उस नगरी के केवल स्मरण मात्र के साथ ही मेरी स्मृतियों के अरण्य में एकदम खलबली मच जाती है और घटनाओं के हरिणों के झुण्ड के झुण्ड छलाँगें मारते हुए दौड़ने लगते हैं। कोई कहता है स्मृतियाँ मयूरपंख जैसी होती हैं, तो किसी का कहना है, वे बकुल के फूल की तरह होती हैं, जो अपनी सुगन्ध को पीछे छोड़ जाते हैं। लेकिन मैं यह स्वीकार नहीं कर सका ! स्मृतियाँ सदैव ही हाथी के पैरों जैसी होती हैं। वे मन की आर्द्र भूमि पर अपना गहरा चिह्न पीछे छोड़ जाती है। कम से कम मेरी तो सभी स्मृतियाँ ऐसी ही हैं। चम्पानगरी मेरे जीवन की मरुभूमि पर कालरूपी गजराज द्वारा अंकित ऐसा ही एक गहरा और स्पष्ट चिह्न है। मेरी जीवन यात्रा में वह सबसे अधिक शान्त और स्पृहणीय लगने वाला आश्रय स्थल है। कुछ लोग जीवन को मन्दिर कहते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा जीवन इस प्रकार का कोई मन्दिर कदापि नहीं है और यदि वह मन्दिर है भी तो चम्पानगरी उस मन्दिर की एकमात्र मधुर घण्टी है।
गंगामाता के विशाल और रमणीय किनारे पर बसा हुआ वह एक छोटा-सा गाँव है। कैसा है वह ?
आज अपने जीवन के उस तरकश को मैं सबके सामने अच्छी तरह खोलकर दिखा देना चाहता हूँ ! उसमें रखे हुए विविध घटनाओं के बाणों को-बिल्कुल एक-सी सभी घटनाओं के बाणों को-मैं मुक्त मन से अपने ही हाथों से सबको दिखा देना चाहता हूँ। अपने दिव्य फलकों से चमचमाते हुए, अपने पौरुष और आकर्षक आकार के कारण तत्क्षण मन को मोह लेने वाले, साथ ही टूटे हुए पुच्छ के कारण दयनीय दिखाई देने वाले तथा जहाँ-तहाँ टूटे हुए फलकों के कारण अटपटे और अजीब-से प्रतीत होने वाले सभी बाणों को-और वे भी जैसे हैं वैसे ही-मैं आज सबको दिखाना चाहता हूँ !
विश्व की श्रेष्ठ वीरता की तुला पर मैं उनकी अच्छी तरह परख कराना चाहता हूँ। धरणीतल के समस्त मातृत्व के द्वारा आज मैं उनका वास्तविक मूल्य निश्चित कराना चाहता हूँ। पृथ्वीतल के एक-एक की गुरुता द्वारा मैं उनका वास्तविक स्थान निर्धारित कराना चाहता हूँ। प्राणों की बाज़ी लगा देने वाली मित्रता के द्वारा मैं आज उनकी परीक्षा कराना चाहता हूँ। हार्दिक फुहारों से भीग जानेवाले बन्धुत्व के द्वारा मैं उनका वास्तविक मूल्यांकन कराना चाहता हूँ।
भीतर से-मेरे मन के एकदम गहन-गम्भीर अन्तरतम से एक आवाज बार-बार मुझको सुनाई देने लगी है। दृढ़ निश्चय के साथ जैसे-जैसे मैं मन ही मन उस आवाज़ को रोकने का प्रयत्न करता हूँ, वैसे-ही-वैसे हवा के तीव्र झोंको से अग्नि की ज्वाला जैसे बुझने के बजाय पहले की अपेक्षा और अधिक जोर से भड़क उठती है, वैसे ही वह आवाज बार-बार गरजकर मुझसे कहती है, ‘‘कहो कर्ण ! अपनी जीवन कथा आज सबको बता दो। वह कथा तुम ऐसी भाषा में कहो कि सब समझ सकें, क्योंकि आज परिस्थिति ही ऐसी है। सारा संसार कह रहा है, ‘कर्ण, तेरा जीवन तो चिथड़े के समान था !’ कहो, गरजकर सबसे कहो कि वह चिथड़ा नहीं था, बल्कि वह तो गोटा किनारवाला एक अतलसी राजवस्त्र था। केवल-परिस्थितियों के निर्दय कँटीले बाड़े में उलझने से ही उसके सहस्त्रों चिथड़े हो गये थे। जिस किसी के हाथ में वे पड़े, उसने मनमाने ढंग से उनका प्रचार किया। और फिर भी तुमको उस राजवस्त्र पर इतना अभिमान क्यों ?’’
वस्तुओं के किसी ढेर में सुन्दर सन्दूक की तह में पड़े हुए नये निकोर और अखण्ड राजवस्त्र की अपेक्षा, भयंकर ताण्डव करने वाले काल के झंझावात से अकेले जूझते हुए चीर-चीर होने वाला यह तेरा राजवस्त्र क्या कम मूल्यवान् था, यह आज सबको आँखें खोलकर अच्छी तरह देख लेने दे ! कान खोलकर अच्छी तरह सुन लेने दे ! वीरों की कहानियाँ सदैव ही बड़ी रुचि से सुननेवाले तथा दूसरे ही क्षण-एकदम दूसरे ही क्षण उतनी ही सरलता और निश्चिन्तता से बिलकुल ही भूल जानेवाले इस पागल संसार को तेरी यह कहानी क्या कभी ज़ोर से झकझोर सकेगी ? क्या उसमें इतनी प्रचण्ड शक्ति है ?
विश्व की चरम सत्यता पर जिनका अखण्ड विश्वास है, जो लोग मृत्यु को एक खिलौना समझते है, सिंह की-सी छाती वाले जिन वीरों का इस धराधाम पर अस्तित्व है, वे सभी लोग आज तुम्हारी कहानी को सुनना चाहेंगे। आह ! यह क्या केवल कहानी है ? यह तो एक महान् सत्य है। और सत्य देखने वालों की और सुनने वालों की इच्छा का विचार कभी नहीं किया जाता। वह सदैव जिसरूप में होता है, उसी रूप में सामने आया करता है उदित होते हुए सूर्यदेव की तरह।
कथा कोई भी हो, उसको सुनते समय श्रोता यह आशा करते हैं कि उसमें मदिरा के मधुर चषक होंगे ! नर्तकियों का नादमय पदन्यास होंगे और होंगे स्त्री-पुरुष के आवेग पूर्ण आलिंगन ! वे उसमें एक ऐसा नशा चाहते हैं जो क्षणभंगुर जीवन की प्रतीति को एकदम भुला दे। जो कहानी मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी उस जीवन गाथा में मदिरा के ऐसे चषक नहीं है। मन को धीरे से गुदगुदाने वाले नर्तकियों के पदन्यास भी नहीं है उसमें है केवल संग्राम। भिन्न-भिन्न प्रकार के भावों को कँपा देने वाला संग्राम !
मैं तो तन-मन से लड़ने वाला केवल एक असभ्य सैनिक हूँ। मैं अपनी कहानी आज अपने केवल अपने ही समाधान के लिए कह रहा हूँ। मनुष्य अपने मन की बात जब तक कहीं कह नहीं लेता, तब तक उसका मन हलका ही नहीं होता। इसलिए मैं अपनी यह कहानी मुक्त मन से कहने जा रहा हूँ।
लेकिन अब मेरे सामने वास्तविक कठिनाई तो यह है कि अपनी इस संग्राम-कथा को मैं काल-क्रमानुसार कैसे कहूँ ? क्योंकि, कड़कड़ाती हुई बिजली की कानों के परदे फाड़ डालने वाली मर्मभेदी आवाज़ सुनकर वन्य घोड़ों के झुण्ड के अनेक घोड़े जैसे जिधर रास्ता मिलता है, उधर ही दौड़ने लगते हैं; वैसे ही अनेक घटनाएँ इस समय मेरी आँखों के सामने कालक्रम को छोड़कर इधर-उधर मनचाही दौड़ लगा रही हैं उनको कालक्रमानुसार कैसे जोड़ूँ, यह स्वयं मुझे भी नहीं सूझ रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस समय बार-बार मेरी आँखों के सामने जो खड़ी हो रही है, वह है गंगामाता के पवित्र और रमणीय तीर पर बसी हुई चम्पानगरी। चम्पानगरी मेरी जीवन सरिता का वह सुन्दर मोड़ है, जो मुझको ही प्रिय लगता है।
उस नगरी के केवल स्मरण मात्र के साथ ही मेरी स्मृतियों के अरण्य में एकदम खलबली मच जाती है और घटनाओं के हरिणों के झुण्ड के झुण्ड छलाँगें मारते हुए दौड़ने लगते हैं। कोई कहता है स्मृतियाँ मयूरपंख जैसी होती हैं, तो किसी का कहना है, वे बकुल के फूल की तरह होती हैं, जो अपनी सुगन्ध को पीछे छोड़ जाते हैं। लेकिन मैं यह स्वीकार नहीं कर सका ! स्मृतियाँ सदैव ही हाथी के पैरों जैसी होती हैं। वे मन की आर्द्र भूमि पर अपना गहरा चिह्न पीछे छोड़ जाती है। कम से कम मेरी तो सभी स्मृतियाँ ऐसी ही हैं। चम्पानगरी मेरे जीवन की मरुभूमि पर कालरूपी गजराज द्वारा अंकित ऐसा ही एक गहरा और स्पष्ट चिह्न है। मेरी जीवन यात्रा में वह सबसे अधिक शान्त और स्पृहणीय लगने वाला आश्रय स्थल है। कुछ लोग जीवन को मन्दिर कहते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा जीवन इस प्रकार का कोई मन्दिर कदापि नहीं है और यदि वह मन्दिर है भी तो चम्पानगरी उस मन्दिर की एकमात्र मधुर घण्टी है।
गंगामाता के विशाल और रमणीय किनारे पर बसा हुआ वह एक छोटा-सा गाँव है। कैसा है वह ?
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book