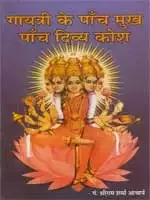|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> गायत्री के पाँच मुख पाँच दिव्य कोश गायत्री के पाँच मुख पाँच दिव्य कोशश्रीराम शर्मा आचार्य
|
225 पाठक हैं |
||||||
गायत्री के पांच मुख पाँच दिव्य कोश
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
गायत्री के पाँच मुख-पाँच दिव्य कोश
गायत्री के पंचमुखी चित्रों एवं पंचमुखी प्रतिभाओं का प्रचलन इसी प्रयोजन
के लिए है कि इस महामंत्र की साधना का अवलंबन करने वालों को यह विदित रहे
कि हमें आगे चलकर क्या करना है ? जप, ध्यान, स्रोत, पाठ-पूजन, हवन, ये
आरम्भिक क्रिया-कृत्य हैं। इनसे शरीर की शुद्धि और मन की एकाग्रता का
प्रारंभिक प्रयोजन पूरा होता है। इससे अंगली मंजिलें कड़ी हैं। उनकी
पूर्ति के लिए साधक को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उस मार्ग पर चलने के
लिए आवश्यक तत्परता, दृढ़ता एवं क्षमता का संपादन करना चाहिए। इतना स्मरण
यदि साधक रख सका तो, समझना चाहिए कि उसने गायत्री पंचमुखी चित्रण का
प्रयोजन ठीक तरह से समझ लिया है।
वस्तुत: गायत्री परमब्रह्म परमात्मा की विश्वव्यापी महाशक्ति उसका कोई स्वरूप नहीं। यदि स्वरूप का आभास पाना हो, तो वह प्रकाश रूप में हो सकता है। ज्ञान की उपमा प्रकाश से दी जाती है, गायत्री का देवता सविता है। सविता का अर्थ है सूर्य-प्रकाश पुंज। जब गायत्री महाशक्ति का अवतरण साधक में होता है, तो साधक को ध्यान के समय प्रकाश बिन्दु एवं वृत्त का आभास मिलता है। उसे अपने हृदय, सिर, नाभि अथवा आँखों में छोटा या बड़ा प्रकाश पिंड दिखाई पड़ता है। वह कभी घटता, कभी बढ़ता है। इसमें कई तरह की कई आकृतियाँ भी, कई रंगों की प्रकाश किरणें दृष्टिगोचर होती है। ये आरंभ में हिलती -डुलती-रहती है, कभी प्रकट कभी लुप्त होती है, पर धीरे- धीरे वह स्थिति आ जाती है कि विभिन्न आकृतियाँ हलचलें एवं रंगों का निराकरण हो जाता है और केवल प्रकाश बिन्दु ही शेष रह जाता है।
प्राथमिक स्थिति में यह प्रकाश छोटे आकार का एवं स्वल्प तेज का होता है, किन्तु जैसे-जैसे आत्मिक प्रगति उर्ध्वगामी होती है वैसे-वैसे प्रकाश वृत्त बड़े आकार का, अधिक प्रकाश का, अधिक उल्लास भरा दिखता है। जैसे प्रात: काल के उगते हुए सूर्य की गर्मी पाकर कमल की कलियाँ खिल पड़ती हैं, वैसे ही अंतरात्मा इस प्रकाश-अनुभूति को देखकर बह्मानन्द का, परमानंद का, सच्चिदानंद का अनुभव करता है। जिस प्रकार चकोर रात भर चन्द्रमा को देखता रहता है वैसे ही साधक की इच्छा होती है कि वह इस प्रकाश को ही देखकर आनंद विभोर होता रहे। कई बार ऐसी भावना ही उठती है कि जिस प्रकार दीपक पर पतंगा अपना प्राण होम देता है, अपनी तुच्छ सत्ता को प्रकाश की महत्ता में विलीन होने का उपक्रम करता है, वैसे ही मैं भी अपने अह्म को इस प्रकाश रूप ब्रह्म में लीन कर दूँ।
यह निराकार ब्रह्म के ध्यान की थोड़ी झाँकी हुई। अनुभूति की दृष्टि से साधक को ऐसा भान होता है, मानो उसे ब्रह्म-ज्ञान की, तत्त्वदर्शन की अनुभूति हो रही हो, ज्ञान के सारांश का जो निष्कर्ष है, उत्कृष्ट आदर्शवाद क्रिया-कलाप से जीवन को ओत-प्रोत कर लेना, वहीं आकांक्षा एवं प्रेरणा मेरे भीतर जाग रही है। जागरण ही नहीं, वरन् संकल्प के निश्चय का, अवस्था का तथ्य का रूप धारण कर रही है। प्रकाश की अनुभूति का यही चिह्न है। माया-मोह और स्वार्थ-संकीर्णता का अज्ञान तिरोहति होने से मनुष्य विशाल दृष्टिकोण से सोचता है और महान आत्माओं जैसी साहसपूर्ण गतिविधियाँ अपनाता है, उसे लोभी और स्वार्थी, मोहग्रस्त, मायाबद्ध लोगों की तरह परमार्थ पथ में साहसपूर्ण कदम बढ़ाते हुए न तो झिझक लगती है और न संकोच होता है। जो उचित है उसे करने के लिए, अपनाने के लिए निर्भीकतापूर्वक साहस भरे कदम उठाता हुआ श्रेय पथ पर अग्रसर होने के लिए द्रुतगति से बढ़ चलता है।
यह तो गायत्री रूपी परमब्रह्म सत्ता के उच्चस्तरीय ज्ञान एवं ध्यान का स्वरूप हुआ। प्रारम्भिक स्थिति में ऐसी उच्चस्तरीय अनुभूतियाँ संभव नहीं उस दशा में प्रारम्भिक क्रम ही चलाना पड़ता है। जप, पूजन, ध्यान, स्तवन, हवन जैसे शरीर साध्य क्रिया-कलाप ही प्रयोग में आते हैं। तब चित्र या प्रतिमा का अवलंबन ग्रहण किये बिना काम नहीं चलता। प्रारंभिक उपासना, साकार माध्यम से ही संभव है। निराकार का स्तर काफी ऊँचे उठ जाने पर आता है। उस स्थिति में भी प्रतिमा का विरोध या परित्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन् उसे नित्य कर्म में सम्मिलित रखकर संचित संस्कार को बनाए रखना पड़ता है। इमारत की नींव में कंकड़-पत्थर भरे जाते हैं।
नीव जम जाने पर तरह-तरह की डिजायनों की इमारतें उस पर खड़ी होती हैं। नींव में पड़े हुए कंकड़-पत्थर दृष्टि से ओझल हो जाते हैं- फिर भी उनका उपहास उड़ाने, परित्याग करने या निकाल फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वरन् यह मानना पड़ता है कि उस विशाल एवं बहुमूल्य इमारत का आधार, वे नींव में भरे हुए कंकड़-पत्थर ही हैं। साकार उपासना की आध्यात्मिक प्रगति को भी नींव भरना कहा जा सकता है। आरंभिक स्थिति में उसकी अनिवार्य आवश्यकता ही मानी गई है। अस्तु, अध्यात्म का आरम्भ चिर अतीत से प्रतिमा पूजन के सहारे हुआ है और क्रमश: आगे बढ़ता चला गया है। गायत्री महाशक्ति की आकृति की निर्धारण भी इसी संदर्भ में हुआ है। अन्य देव प्रतिमाओं की तरह उसका विग्रह भी आदिकाल से ही ध्यान एवं पूजन में प्रयुक्त होता रहा है।
सामान्यता एक मुख और दो भुजा वाली मानव आकृति की प्रतिमा ही उपयुक्त है। पूजन और ध्यान उसी का ठीक बनता है। सगी माता मानने के लिए गायत्री को भी वैसे ही हाथ-पैर वाली होना चाहिए जैसा कि साधक का होता है। इसलिए ध्यान एवं पूजन में सदा से दो भुजाओं वाली और एक मुख वाली पुस्तक एवं कमंडल धारण करनेवाली हंसवाहिनी गायत्री माता का प्रयोग होता रहा है। किन्तु कतिपय स्थानों में पंचमुखी प्रतिमा एवं चित्र भी देखे जाते हैं। इनका ध्यान-पूजन भले ही उपयुक्त न हो, पर उसमें एक महत्त्वपूर्ण शिक्षण संदेश एवं निर्देश ही भरा हुआ है। हमें उसी को देखना-समझना चाहिए।
गायत्री के पाँच मुख, जीव के ऊपर लिपटे हुए पंच-कोश-पाँच आवरण हैं और दस भुजाएँ, दस सिद्धियाँ एवं अनुभूतियाँ हैं। पाँच भुजाएँ बाईं ओर पाँच भुजाएँ दाहिनी ओर हैं। उसका संकेत गायत्री महाशक्ति के साथ जुड़ी हुई पाँच भौतिक और पाँच अध्यात्मिक शक्तियों एवं सिद्धियों की ओर है।
इस महाशक्ति का अवतरण जहाँ भी होगा, वहाँ वे दस अनुभूतियाँ-विशेषताएँ- संपदाएँ निश्चित रूप से परिलक्षित होंगी। साधाना का अर्थ एक नियत पूजा स्थान पर बैठकर अमुक क्रिया-कलाप पूरा कर लेना मात्र ही नहीं है, वरन् समस्त जीवन को साधनामय बनाकर अपने गुण, कर्म, स्वभाव का इतने उत्कृष्ट स्तर का बनाना है कि उसमें वे विभूतियाँ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगें, जिनका संकेत पंचमुखी माता की प्रतिमा की प्रतीक से है। साधना का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है। दस शक्तियाँ दस सिद्धियाँ जीवन साधना के द्वारा जब प्राप्त की जाने लगें, तो समझना चाहिए कि कोई गायत्री उपासक उच्चस्तरीय साधन-पथ पर सफलतापूर्वक अग्रसर हो रहा है।
गायत्री के पाँच मुख हमें बताते हैं कि जीव सत्ता के साथ पाँच सशक्त देवता, उसके लक्ष्य प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए मिले हुए हैं। ये निद्राग्रस्त हो जाने के कारण मृततुल्य पड़े रहते हैं और किसी काम नहीं आते। फलत: जीव दीन-दुर्बल बना रहता है। यदि इन सशक्त सहायकों को जगाया जा सके, उनकी सामर्थ्य का उपयोग किया जा सके, तो मनुष्य सामान्य न रहकर असामान्य बनेगा। दुर्दशाग्रस्त स्थिति से उबरने और अपने महान् गौरव के अनुरूप जीवनयापन का अवसर मिलेगा। शरीरगत पाँच तत्त्वों का उल्लेख पाँच देवताओं के रूप में किया गया है-
वस्तुत: गायत्री परमब्रह्म परमात्मा की विश्वव्यापी महाशक्ति उसका कोई स्वरूप नहीं। यदि स्वरूप का आभास पाना हो, तो वह प्रकाश रूप में हो सकता है। ज्ञान की उपमा प्रकाश से दी जाती है, गायत्री का देवता सविता है। सविता का अर्थ है सूर्य-प्रकाश पुंज। जब गायत्री महाशक्ति का अवतरण साधक में होता है, तो साधक को ध्यान के समय प्रकाश बिन्दु एवं वृत्त का आभास मिलता है। उसे अपने हृदय, सिर, नाभि अथवा आँखों में छोटा या बड़ा प्रकाश पिंड दिखाई पड़ता है। वह कभी घटता, कभी बढ़ता है। इसमें कई तरह की कई आकृतियाँ भी, कई रंगों की प्रकाश किरणें दृष्टिगोचर होती है। ये आरंभ में हिलती -डुलती-रहती है, कभी प्रकट कभी लुप्त होती है, पर धीरे- धीरे वह स्थिति आ जाती है कि विभिन्न आकृतियाँ हलचलें एवं रंगों का निराकरण हो जाता है और केवल प्रकाश बिन्दु ही शेष रह जाता है।
प्राथमिक स्थिति में यह प्रकाश छोटे आकार का एवं स्वल्प तेज का होता है, किन्तु जैसे-जैसे आत्मिक प्रगति उर्ध्वगामी होती है वैसे-वैसे प्रकाश वृत्त बड़े आकार का, अधिक प्रकाश का, अधिक उल्लास भरा दिखता है। जैसे प्रात: काल के उगते हुए सूर्य की गर्मी पाकर कमल की कलियाँ खिल पड़ती हैं, वैसे ही अंतरात्मा इस प्रकाश-अनुभूति को देखकर बह्मानन्द का, परमानंद का, सच्चिदानंद का अनुभव करता है। जिस प्रकार चकोर रात भर चन्द्रमा को देखता रहता है वैसे ही साधक की इच्छा होती है कि वह इस प्रकाश को ही देखकर आनंद विभोर होता रहे। कई बार ऐसी भावना ही उठती है कि जिस प्रकार दीपक पर पतंगा अपना प्राण होम देता है, अपनी तुच्छ सत्ता को प्रकाश की महत्ता में विलीन होने का उपक्रम करता है, वैसे ही मैं भी अपने अह्म को इस प्रकाश रूप ब्रह्म में लीन कर दूँ।
यह निराकार ब्रह्म के ध्यान की थोड़ी झाँकी हुई। अनुभूति की दृष्टि से साधक को ऐसा भान होता है, मानो उसे ब्रह्म-ज्ञान की, तत्त्वदर्शन की अनुभूति हो रही हो, ज्ञान के सारांश का जो निष्कर्ष है, उत्कृष्ट आदर्शवाद क्रिया-कलाप से जीवन को ओत-प्रोत कर लेना, वहीं आकांक्षा एवं प्रेरणा मेरे भीतर जाग रही है। जागरण ही नहीं, वरन् संकल्प के निश्चय का, अवस्था का तथ्य का रूप धारण कर रही है। प्रकाश की अनुभूति का यही चिह्न है। माया-मोह और स्वार्थ-संकीर्णता का अज्ञान तिरोहति होने से मनुष्य विशाल दृष्टिकोण से सोचता है और महान आत्माओं जैसी साहसपूर्ण गतिविधियाँ अपनाता है, उसे लोभी और स्वार्थी, मोहग्रस्त, मायाबद्ध लोगों की तरह परमार्थ पथ में साहसपूर्ण कदम बढ़ाते हुए न तो झिझक लगती है और न संकोच होता है। जो उचित है उसे करने के लिए, अपनाने के लिए निर्भीकतापूर्वक साहस भरे कदम उठाता हुआ श्रेय पथ पर अग्रसर होने के लिए द्रुतगति से बढ़ चलता है।
यह तो गायत्री रूपी परमब्रह्म सत्ता के उच्चस्तरीय ज्ञान एवं ध्यान का स्वरूप हुआ। प्रारम्भिक स्थिति में ऐसी उच्चस्तरीय अनुभूतियाँ संभव नहीं उस दशा में प्रारम्भिक क्रम ही चलाना पड़ता है। जप, पूजन, ध्यान, स्तवन, हवन जैसे शरीर साध्य क्रिया-कलाप ही प्रयोग में आते हैं। तब चित्र या प्रतिमा का अवलंबन ग्रहण किये बिना काम नहीं चलता। प्रारंभिक उपासना, साकार माध्यम से ही संभव है। निराकार का स्तर काफी ऊँचे उठ जाने पर आता है। उस स्थिति में भी प्रतिमा का विरोध या परित्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन् उसे नित्य कर्म में सम्मिलित रखकर संचित संस्कार को बनाए रखना पड़ता है। इमारत की नींव में कंकड़-पत्थर भरे जाते हैं।
नीव जम जाने पर तरह-तरह की डिजायनों की इमारतें उस पर खड़ी होती हैं। नींव में पड़े हुए कंकड़-पत्थर दृष्टि से ओझल हो जाते हैं- फिर भी उनका उपहास उड़ाने, परित्याग करने या निकाल फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वरन् यह मानना पड़ता है कि उस विशाल एवं बहुमूल्य इमारत का आधार, वे नींव में भरे हुए कंकड़-पत्थर ही हैं। साकार उपासना की आध्यात्मिक प्रगति को भी नींव भरना कहा जा सकता है। आरंभिक स्थिति में उसकी अनिवार्य आवश्यकता ही मानी गई है। अस्तु, अध्यात्म का आरम्भ चिर अतीत से प्रतिमा पूजन के सहारे हुआ है और क्रमश: आगे बढ़ता चला गया है। गायत्री महाशक्ति की आकृति की निर्धारण भी इसी संदर्भ में हुआ है। अन्य देव प्रतिमाओं की तरह उसका विग्रह भी आदिकाल से ही ध्यान एवं पूजन में प्रयुक्त होता रहा है।
सामान्यता एक मुख और दो भुजा वाली मानव आकृति की प्रतिमा ही उपयुक्त है। पूजन और ध्यान उसी का ठीक बनता है। सगी माता मानने के लिए गायत्री को भी वैसे ही हाथ-पैर वाली होना चाहिए जैसा कि साधक का होता है। इसलिए ध्यान एवं पूजन में सदा से दो भुजाओं वाली और एक मुख वाली पुस्तक एवं कमंडल धारण करनेवाली हंसवाहिनी गायत्री माता का प्रयोग होता रहा है। किन्तु कतिपय स्थानों में पंचमुखी प्रतिमा एवं चित्र भी देखे जाते हैं। इनका ध्यान-पूजन भले ही उपयुक्त न हो, पर उसमें एक महत्त्वपूर्ण शिक्षण संदेश एवं निर्देश ही भरा हुआ है। हमें उसी को देखना-समझना चाहिए।
गायत्री के पाँच मुख, जीव के ऊपर लिपटे हुए पंच-कोश-पाँच आवरण हैं और दस भुजाएँ, दस सिद्धियाँ एवं अनुभूतियाँ हैं। पाँच भुजाएँ बाईं ओर पाँच भुजाएँ दाहिनी ओर हैं। उसका संकेत गायत्री महाशक्ति के साथ जुड़ी हुई पाँच भौतिक और पाँच अध्यात्मिक शक्तियों एवं सिद्धियों की ओर है।
इस महाशक्ति का अवतरण जहाँ भी होगा, वहाँ वे दस अनुभूतियाँ-विशेषताएँ- संपदाएँ निश्चित रूप से परिलक्षित होंगी। साधाना का अर्थ एक नियत पूजा स्थान पर बैठकर अमुक क्रिया-कलाप पूरा कर लेना मात्र ही नहीं है, वरन् समस्त जीवन को साधनामय बनाकर अपने गुण, कर्म, स्वभाव का इतने उत्कृष्ट स्तर का बनाना है कि उसमें वे विभूतियाँ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगें, जिनका संकेत पंचमुखी माता की प्रतिमा की प्रतीक से है। साधना का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है। दस शक्तियाँ दस सिद्धियाँ जीवन साधना के द्वारा जब प्राप्त की जाने लगें, तो समझना चाहिए कि कोई गायत्री उपासक उच्चस्तरीय साधन-पथ पर सफलतापूर्वक अग्रसर हो रहा है।
गायत्री के पाँच मुख हमें बताते हैं कि जीव सत्ता के साथ पाँच सशक्त देवता, उसके लक्ष्य प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए मिले हुए हैं। ये निद्राग्रस्त हो जाने के कारण मृततुल्य पड़े रहते हैं और किसी काम नहीं आते। फलत: जीव दीन-दुर्बल बना रहता है। यदि इन सशक्त सहायकों को जगाया जा सके, उनकी सामर्थ्य का उपयोग किया जा सके, तो मनुष्य सामान्य न रहकर असामान्य बनेगा। दुर्दशाग्रस्त स्थिति से उबरने और अपने महान् गौरव के अनुरूप जीवनयापन का अवसर मिलेगा। शरीरगत पाँच तत्त्वों का उल्लेख पाँच देवताओं के रूप में किया गया है-
‘‘आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेश्चैव महेश्वर:।
वायो: सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य मणाधिप:।।
वायो: सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य मणाधिप:।।
कपिलतंत्र
आकाश के अधिपति है विष्णु। अग्नि की अधपति महेश्वरी शक्ति है। वायु के
अधिपति सूर्य हैं। पृथ्वी के स्वामी शिव हैं और जल के अधिपति गणेश जी हैं।
इस प्रकार पंच देव शरीर के पंचतत्त्वों की ही अधपति-सत्ताएँ हैं।
पाँच प्राणों को भी पाँच देव बताया गया है।
पाँच प्राणों को भी पाँच देव बताया गया है।
पंचदेव मय जीव: पंच प्राणमयं शिव:।
कुंडली शक्ति संयुक्तं, शुभ्र विद्युल्लतोपमम्।।
कुंडली शक्ति संयुक्तं, शुभ्र विद्युल्लतोपमम्।।
तंत्रार्णव
ये जीव पाँच देव सहित है। प्राणवान् होने पर शिव है। यह परिकर कुंडलिनी
शक्ति युक्त है। इनका आकार चमकती बिजली के समान है।
कुंडलिनी जागरण का परिचय पंच कोशों की जाग्रति के रूप में मिलता है।
कुंडलिनी जागरण का परिचय पंच कोशों की जाग्रति के रूप में मिलता है।
कुंडलिनी शक्तिराविर्भवति साधके।
तदा स पंच कोशेषु मत्तेजोऽनुभवति ध्रुवम्।।
तदा स पंच कोशेषु मत्तेजोऽनुभवति ध्रुवम्।।
महायोग
विज्ञान
जब कुंडलिनी जाग्रत होती है, तो साधक के पाँचों कोश ज्योतिर्मय हो उठते
हैं।
पाँच तत्त्वों से शरीर बना है। उसके सत्त्व गुण चेतना के पाँच उभारों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं।
(1) मन: माइंड
(2) बुद्धि: इंटिलेक्ट
(3) इच्छा: विल
(4) चित्त: माइंड स्टफ
(5) अहंकार: ईगो।
पाँच तत्त्वों से शरीर बना है। उसके सत्त्व गुण चेतना के पाँच उभारों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं।
(1) मन: माइंड
(2) बुद्धि: इंटिलेक्ट
(3) इच्छा: विल
(4) चित्त: माइंड स्टफ
(5) अहंकार: ईगो।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book