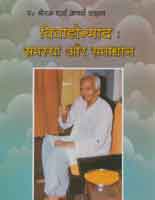|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> विवाहोन्माद समस्या और समाधान विवाहोन्माद समस्या और समाधानश्रीराम शर्मा आचार्य
|
431 पाठक हैं |
||||||
विवाहोन्माद समस्या और समाधान....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
समर्पणम्
ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामञ्ञ जगद्गुरुम्।
पादपद्मे तयो: श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुह:।।
मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका।
नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा-प्रज्ञा युता च या।।
भगवत्या: जगन्मातु:, श्रीरामस्य जगद्गुरो:।
पादुकायुगले वन्दे, श्रद्धाप्रज्ञास्वरूपयो:।।
नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा।
यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्।।
असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतिरोधसक्षमम्।
युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्।।
त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये।
पादपद्मे तयो: श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुह:।।
मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका।
नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा-प्रज्ञा युता च या।।
भगवत्या: जगन्मातु:, श्रीरामस्य जगद्गुरो:।
पादुकायुगले वन्दे, श्रद्धाप्रज्ञास्वरूपयो:।।
नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा।
यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्।।
असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतिरोधसक्षमम्।
युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्।।
त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये।
भूमिका
विवाह एक पवित्र बन्धन है। दो आत्माओं का मिलन है। इसके माध्यम से नर और
नारी मिलकर एक परिपूर्ण व्यक्तित्व की, एक गृहस्थ संस्था की स्थापना करते
हैं। किसी भी समाज में वर्जनाओं को बनाए रखने तथा नैतिक मूल्यों का आधार
सुदृढ़ बनाने के लिए विवाह एक कर्त्तव्य बंधन के रूप में अनिवार्य माना
जाता है। यह इस बंधन के शुभारंभ की, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की सार्वजनिक
घोषणा है। स्वाभाविक है कि ऐसे प्रसंग पर सभी को प्रसन्नता हो, सभी
कुटुम्बीजन सार्वजनिक रूप से अपने हर्ष की अभिव्यक्ति करें, इसीलिए
हर्षोत्सव के रूप में एक संक्षिप्त-सा समारोह हर जाति, धर्म, सम्प्रदाय
में ऐसे अवसरों पर मना लिया जाता है। विवाहोत्सव के तरीके अलग-अलग हो सकते
हैं पर हर्षाभिव्यक्ति के रूप में यह मनाया प्राय: सभी देशों-वर्गों में
जाता है।
हिन्दू समाज में यह विवाहोत्सव जिस गरिमा के साथ सम्पन्न होना चाहिए था, जैसा कि भारतीय संस्कृति की अनादि काल से परंपरा रही है, वह न होकर कुछ ऐसे विकृत रूप में अब समाज के समक्ष आ रहा है कि लगता है कि गरीब माना जाने वाला यह राष्ट्र वास्तव में गरीब नहीं है या तो खर्चीली शादियों ने हमें गरीब बनाया है अथवा हम अमेरिका का स्वाँग रचाकर अपने अहं का प्रदर्शन इस उत्सव के माध्यम से करने लगे हैं, जिसने एक उन्माद का रूप अब ले लिया है।
परमपूज्य गुरुदेव जी की वेदना यही है कि विवाह जैसे धर्मकृत्य को, एक पुनीत प्रयोजन को क्यों अपव्यय प्रधान से अहंता से उद्धत नृत्य के रूप में बदल दिया गया। देन-दहेज, तिलक, नेग-चलन, धूमधाम से जिस तरह अधिक खर्च किया जाता है व उसी में बड़प्पन अनुभव किया जाता है, यह हमारे सामाज के लिए धर्म की बात है। जो अपने घर में होने वाली विवाहों में जितना अधिक अपव्यय करता है, उसी अनुपात में उसे बड़ा आदमी माना जाता है, यह एक विडम्बना है। पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा इतनी बढ़ गयी है, कि पहले से दूसरा व दूसरे से तीसरा अधिकाधिक खर्च करता देखा जाता है। अपनी तथाकथित प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व फूँककर भी शादियाँ सम्पन्न की जाती हैं व इसी में बड़प्पन माना जाता है।
हमारे देश में जहाँ तीन चौथाई आबादी रोज कुआँ खोदकर पानी पीने जैसी कहावत चरितार्थ कर अपनी उसी दिन की आजीविका की व्यवस्था करती है तथा अधिकतर व्यक्ति जो मध्यम वर्ग में हैं- वेतन भोगी हैं, व्यापारी हैं उनकी भी ऐसी स्थिति नहीं है, वे इस प्रतिस्पर्द्धा में पिस जाते हैं। औसत भारतीय बचत तब करे जब कमाई बढ़े, व आजीविका के अन्य वैकल्पिक स्रोत्र विकसित हों। वह हो नहीं पाता व लड़की विवाह योग्य हो जाती है। ऐसे में कन्याओं की दुर्गति होना स्वाभाविक है। लड़की वाला वैसे भी हमारे समाज की चली आ रही षड्यंत्रकारी नीति के कारण दीन-हीन, भिक्षुक की तरह गिडगिड़ाता रहता है पर उसकी सुनता कौन है ? लड़के नीलामी की तरह बोली पर चढ़े रहते हैं, अनाप-शनाप माँग होती है एवं वधू पक्ष उसमें पूरी तरह कंगाल हो जाता है। आज बड़ी संख्या में अधेड़ होती जा रही अविवाहित कन्याओं की समस्या इसी विवाहोन्माद के अभिशाप के कारण पैदा हुई है। जब तक लड़के विवाह आमदानी का एक साधन माना जायगा, तब तक वस्तुत: लड़कियों को सताए जाने का क्रम बन्द नहीं होगा। लड़की पक्ष के गरीब व दिवालिए होते चले जाने का सिलसिला रुकेगा नहीं।
बहुसंख्यक व्यक्ति बेईमान होते नहीं। उन्हें आज के सामाजिक प्रचलन जिनमें विवाह का अपव्यय भी कारण है, ऐसा बनने पर मजबूर कर देते हैं। यदि इस नैतिक संकट से हमें जूझना है एवं समाज को हर दृष्टि से सुसंस्कारी, समृद्ध बनाना है तो हमें पुन: विवाह की वैदिक व्यवस्था की ओर लौटना होगा जिसमें बिना किसी आडम्बर के सादगी भरे विवाह सम्पन्न होते थे।
सादगीपूर्ण आदर्श विवाहों में अपना पैसा बचता है, अपने स्नेहीजनों के पैसों की भी बचत होती है तथा दोनों पक्षों में असाधारण प्रेमभाव बना रहता है। बचा हुआ पैसा बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाए रखने में खर्च हो सकता है। भारतीय कन्याओं की आत्माएँ पूज्यवर के अनुसार उन रत्नों की शत-शत आशीर्वादों द्वारा पूजा करेगी जो इस कुप्रथा की पूतना को मार सकें, ताड़का को भगा सकें, सूर्पणखा की नाक काट सकें। समाज के नवनिर्माण की धुरी पर केन्द्रित वाङ्मय का यह खण्ड पूरी तरह विवाह संस्कार- उससे जुड़ी परम्पराओं में आया आडम्बर एवं शुचिता कैसे लायी जाय तथा सफल दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जाय, इसी विषय को समर्पित है। पूज्यवर ने आदर्श विवाहों के, सामूहिक विवाह एक धर्मानुष्ठान के रूप में मनाये जाने के आंदोलन को जन्म दिया एवं प्राय: एक लाख से अधिक ऐसे संस्कारवान दम्पती समाज क्षेत्र को विगत पैंसठ वर्षों में दिए जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह कार्य कैसे गति पकड़े ? कैसे यह एक आन्दोलन का रूप ले ? इसके लिए उनने बड़े विशद् रूप में सबका मार्गदर्शन किया है। जातीय संगठन आगे आकर समाज सेवा के इस कार्य को गति दें, आदर्श विवाहों के अभिनन्दन की एक श्रेष्ठ परम्परा स्थापित हो जाय, इस पर उनने न केवल मार्गदर्शन दिया है अपितु इसे व्यावहारिक बनाते हुए सक्रिय रूप देने का प्रयास भी किया है। पूज्यवर लिखते है कि आदर्श विवाहों की ख्याति दूर-दूर तक फैलनी चाहिए ताकि वैसा करने का उत्साह औरों में भी उत्पन्न हो। विवेकशीलता के जागरण के अभाव में अनेकों व्यक्तियों द्वारा ऐसी आदर्श परम्परा के अवलम्बन का जब व्यापक प्रचार किया जाएगा तो औरों में भी अनुकरण की उमंग जागेगी। इसके लिए वे समाचार पत्रों व मीड़िया के विभिन्न अंगों का अवलम्बन लेने की बात भी कहते हैं एवं प्रतिज्ञा-पत्र भराए जाने के लिए एक सामूहिक मुहिम छेड़ी जाने का उल्लेख भी करते हैं।
समस्या तो निश्चित ही विकट है। बढ़ती आधुनिकता व साधनों के संचय की होड़ में यह और भी विकराल रूप लेती जा रही है। समाधान इसका है एवं वह धर्मतंत्र के माध्यम से ही निकल सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। वाङ्मय के इस खण्ड में समाज निर्माण के क्षेत्र में दिशा दिखाने वाले प्रेरक मार्गदर्शन मात्र ही नहीं, राष्ट्र की समृद्धि का मूल मर्म भी विस्तार से दिया गया है। पढ़ने वाले निश्चित ही न केवल लाभान्वित होंगे, आदर्शवाद के प्रति उनका सम्मान भी बढ़ेगा।
हिन्दू समाज में यह विवाहोत्सव जिस गरिमा के साथ सम्पन्न होना चाहिए था, जैसा कि भारतीय संस्कृति की अनादि काल से परंपरा रही है, वह न होकर कुछ ऐसे विकृत रूप में अब समाज के समक्ष आ रहा है कि लगता है कि गरीब माना जाने वाला यह राष्ट्र वास्तव में गरीब नहीं है या तो खर्चीली शादियों ने हमें गरीब बनाया है अथवा हम अमेरिका का स्वाँग रचाकर अपने अहं का प्रदर्शन इस उत्सव के माध्यम से करने लगे हैं, जिसने एक उन्माद का रूप अब ले लिया है।
परमपूज्य गुरुदेव जी की वेदना यही है कि विवाह जैसे धर्मकृत्य को, एक पुनीत प्रयोजन को क्यों अपव्यय प्रधान से अहंता से उद्धत नृत्य के रूप में बदल दिया गया। देन-दहेज, तिलक, नेग-चलन, धूमधाम से जिस तरह अधिक खर्च किया जाता है व उसी में बड़प्पन अनुभव किया जाता है, यह हमारे सामाज के लिए धर्म की बात है। जो अपने घर में होने वाली विवाहों में जितना अधिक अपव्यय करता है, उसी अनुपात में उसे बड़ा आदमी माना जाता है, यह एक विडम्बना है। पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा इतनी बढ़ गयी है, कि पहले से दूसरा व दूसरे से तीसरा अधिकाधिक खर्च करता देखा जाता है। अपनी तथाकथित प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व फूँककर भी शादियाँ सम्पन्न की जाती हैं व इसी में बड़प्पन माना जाता है।
हमारे देश में जहाँ तीन चौथाई आबादी रोज कुआँ खोदकर पानी पीने जैसी कहावत चरितार्थ कर अपनी उसी दिन की आजीविका की व्यवस्था करती है तथा अधिकतर व्यक्ति जो मध्यम वर्ग में हैं- वेतन भोगी हैं, व्यापारी हैं उनकी भी ऐसी स्थिति नहीं है, वे इस प्रतिस्पर्द्धा में पिस जाते हैं। औसत भारतीय बचत तब करे जब कमाई बढ़े, व आजीविका के अन्य वैकल्पिक स्रोत्र विकसित हों। वह हो नहीं पाता व लड़की विवाह योग्य हो जाती है। ऐसे में कन्याओं की दुर्गति होना स्वाभाविक है। लड़की वाला वैसे भी हमारे समाज की चली आ रही षड्यंत्रकारी नीति के कारण दीन-हीन, भिक्षुक की तरह गिडगिड़ाता रहता है पर उसकी सुनता कौन है ? लड़के नीलामी की तरह बोली पर चढ़े रहते हैं, अनाप-शनाप माँग होती है एवं वधू पक्ष उसमें पूरी तरह कंगाल हो जाता है। आज बड़ी संख्या में अधेड़ होती जा रही अविवाहित कन्याओं की समस्या इसी विवाहोन्माद के अभिशाप के कारण पैदा हुई है। जब तक लड़के विवाह आमदानी का एक साधन माना जायगा, तब तक वस्तुत: लड़कियों को सताए जाने का क्रम बन्द नहीं होगा। लड़की पक्ष के गरीब व दिवालिए होते चले जाने का सिलसिला रुकेगा नहीं।
बहुसंख्यक व्यक्ति बेईमान होते नहीं। उन्हें आज के सामाजिक प्रचलन जिनमें विवाह का अपव्यय भी कारण है, ऐसा बनने पर मजबूर कर देते हैं। यदि इस नैतिक संकट से हमें जूझना है एवं समाज को हर दृष्टि से सुसंस्कारी, समृद्ध बनाना है तो हमें पुन: विवाह की वैदिक व्यवस्था की ओर लौटना होगा जिसमें बिना किसी आडम्बर के सादगी भरे विवाह सम्पन्न होते थे।
सादगीपूर्ण आदर्श विवाहों में अपना पैसा बचता है, अपने स्नेहीजनों के पैसों की भी बचत होती है तथा दोनों पक्षों में असाधारण प्रेमभाव बना रहता है। बचा हुआ पैसा बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाए रखने में खर्च हो सकता है। भारतीय कन्याओं की आत्माएँ पूज्यवर के अनुसार उन रत्नों की शत-शत आशीर्वादों द्वारा पूजा करेगी जो इस कुप्रथा की पूतना को मार सकें, ताड़का को भगा सकें, सूर्पणखा की नाक काट सकें। समाज के नवनिर्माण की धुरी पर केन्द्रित वाङ्मय का यह खण्ड पूरी तरह विवाह संस्कार- उससे जुड़ी परम्पराओं में आया आडम्बर एवं शुचिता कैसे लायी जाय तथा सफल दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जाय, इसी विषय को समर्पित है। पूज्यवर ने आदर्श विवाहों के, सामूहिक विवाह एक धर्मानुष्ठान के रूप में मनाये जाने के आंदोलन को जन्म दिया एवं प्राय: एक लाख से अधिक ऐसे संस्कारवान दम्पती समाज क्षेत्र को विगत पैंसठ वर्षों में दिए जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह कार्य कैसे गति पकड़े ? कैसे यह एक आन्दोलन का रूप ले ? इसके लिए उनने बड़े विशद् रूप में सबका मार्गदर्शन किया है। जातीय संगठन आगे आकर समाज सेवा के इस कार्य को गति दें, आदर्श विवाहों के अभिनन्दन की एक श्रेष्ठ परम्परा स्थापित हो जाय, इस पर उनने न केवल मार्गदर्शन दिया है अपितु इसे व्यावहारिक बनाते हुए सक्रिय रूप देने का प्रयास भी किया है। पूज्यवर लिखते है कि आदर्श विवाहों की ख्याति दूर-दूर तक फैलनी चाहिए ताकि वैसा करने का उत्साह औरों में भी उत्पन्न हो। विवेकशीलता के जागरण के अभाव में अनेकों व्यक्तियों द्वारा ऐसी आदर्श परम्परा के अवलम्बन का जब व्यापक प्रचार किया जाएगा तो औरों में भी अनुकरण की उमंग जागेगी। इसके लिए वे समाचार पत्रों व मीड़िया के विभिन्न अंगों का अवलम्बन लेने की बात भी कहते हैं एवं प्रतिज्ञा-पत्र भराए जाने के लिए एक सामूहिक मुहिम छेड़ी जाने का उल्लेख भी करते हैं।
समस्या तो निश्चित ही विकट है। बढ़ती आधुनिकता व साधनों के संचय की होड़ में यह और भी विकराल रूप लेती जा रही है। समाधान इसका है एवं वह धर्मतंत्र के माध्यम से ही निकल सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। वाङ्मय के इस खण्ड में समाज निर्माण के क्षेत्र में दिशा दिखाने वाले प्रेरक मार्गदर्शन मात्र ही नहीं, राष्ट्र की समृद्धि का मूल मर्म भी विस्तार से दिया गया है। पढ़ने वाले निश्चित ही न केवल लाभान्वित होंगे, आदर्शवाद के प्रति उनका सम्मान भी बढ़ेगा।
ब्रह्मवर्चस
भारतीय संस्कृति की अनुपम देन- विवाह संस्कार
हिन्दू संस्कृति में विवाह का उद्देश्य
संसार की अन्य जातियों की अपेक्षा हिन्दू जाति की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं।
इसका आधार आध्यात्मिक है। ऋषि अपनी लम्बी खोज के परिणामस्वरूप इस निर्णय
पर पहुँचे थे कि सच्ची सुख-शान्ति और आनन्द आध्यात्मिकता में ही है। इसलिए
उन्होंने हिन्दू जाति के प्रत्येक क्रिया-कलाप, आचार व्यवहार एवं चेष्टा
में इस तत्त्व का विशेष स्थान रखा। यही कारण है कि हमारी छोटी से छोटी
क्रिया में भी धर्म का दखल हैं। हमारी खान-पान, मलमूत्र त्याग, सोना-उठना
आदि सभी शारीरिक और मांनसिक, बौद्धिक क्रियाएँ धर्म द्वारा नियंत्रित की
गई हैं ताकि इनको भी हम ठीक ढंग से करें और जैसा करना चाहिए, उससे नीचे न
गिरें और मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के
लिए आगे बढ़ सकें। हमारे वेदशास्त्रों का प्रयास इसी उद्देश्य
की
पूर्ति के लिए है। ऊँचे आदर्शों को लेकर चलने के कारण ही संसार की सभी
सभ्य जातियों में इसका हमेशा ऊँचा स्थान रहा है। विवाह के संबंध में भी
यही बात लागू होती है क्योंकि हिन्दू धर्म में विवाह का उद्देश्य
काम-वासना की तृप्ति नहीं वरन् मनुष्य जीवन की अपूर्णता को दूर करके
पूर्णता की ओर कदम बढ़ाना है। विवाह में प्रयोग आने वाले मंत्र हमें इसी
ओर संकेत करते हैं।
यह तो मानना ही पड़ेगा की सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा ने स्त्री और पुरुष में कुछ ऐसे आकर्षण उत्पन्न किये हैं जिससे वह एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस सृष्टि का क्रम तो चलना ही है, उनमें वह स्वाभाविक काम-प्रवृत्तियाँ तो जाग्रत होंगी ही और हिन्दू धर्म की मान्यता के अनुसार मनुष्य जन्म 84 लाख पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि योनियों के पश्चात् होता है और वह पशु प्रवृत्तियाँ उसमें रहती ही हैं, इसलिए जिस प्रकार से पशु को स्वच्छन्द छोड़ देने से वह किसी भी खेत में चरता रहता है, इसी तरह मनुष्य भी स्वच्छ्न्दता प्राप्त करके अपनी स्वाभाविक कामवासना को शान्त करने के लिए अनियंत्रित हो जायेगा और स्त्रियों के लिए पुरुष के हृदय में और पुरुष के लिए स्त्रियों के हृदय में अनुचित आकर्षण की भावना जाग उठेगी और अवसर मिलने पर वह अपनी पशु-प्रवृत्ति को चरितार्थ करेगा।
इस पद्धति को नियंत्रित करने के लिए ही विवाह की व्यवस्था की गई कि पुरुष एक स्त्री तक सीमित रहे और संसार की अन्य स्त्रियों को पवित्र दृष्टि से देखे। इस प्रकार से विवाह वह पुनीत संस्कार है जिसने मानव को मानव बनाने का कार्य किया है और उसकी पशु-प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लगा दिये हैं। इसके अभाव में मनुष्य पशु से गया-गुजरा होता। न उसकी कोई पत्नी होती, न माँ, न बहिन न बेटी। अपनी कामवासना की पूर्ति के लिए वह कुत्तों की तरह लड़ता, झगड़ता और छीना-झपटी करता। हिन्दू धर्म के अनुसार होने वाले विवाह में प्रयोग में आने वाले मंत्रों द्वारा कन्या यह कहती है कि- ‘‘तुम कभी पर-स्त्री का चिन्तन नहीं करोंगे और मैं पति-परायण होकर तुम्हारे ही साथ निर्वाह करूँगी। तुम्हारे सिवा अन्य किसी पुरुष को पुरुष ही नहीं समझूँगी।’’
यह तो मानना ही पड़ेगा की सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा ने स्त्री और पुरुष में कुछ ऐसे आकर्षण उत्पन्न किये हैं जिससे वह एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस सृष्टि का क्रम तो चलना ही है, उनमें वह स्वाभाविक काम-प्रवृत्तियाँ तो जाग्रत होंगी ही और हिन्दू धर्म की मान्यता के अनुसार मनुष्य जन्म 84 लाख पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि योनियों के पश्चात् होता है और वह पशु प्रवृत्तियाँ उसमें रहती ही हैं, इसलिए जिस प्रकार से पशु को स्वच्छन्द छोड़ देने से वह किसी भी खेत में चरता रहता है, इसी तरह मनुष्य भी स्वच्छ्न्दता प्राप्त करके अपनी स्वाभाविक कामवासना को शान्त करने के लिए अनियंत्रित हो जायेगा और स्त्रियों के लिए पुरुष के हृदय में और पुरुष के लिए स्त्रियों के हृदय में अनुचित आकर्षण की भावना जाग उठेगी और अवसर मिलने पर वह अपनी पशु-प्रवृत्ति को चरितार्थ करेगा।
इस पद्धति को नियंत्रित करने के लिए ही विवाह की व्यवस्था की गई कि पुरुष एक स्त्री तक सीमित रहे और संसार की अन्य स्त्रियों को पवित्र दृष्टि से देखे। इस प्रकार से विवाह वह पुनीत संस्कार है जिसने मानव को मानव बनाने का कार्य किया है और उसकी पशु-प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लगा दिये हैं। इसके अभाव में मनुष्य पशु से गया-गुजरा होता। न उसकी कोई पत्नी होती, न माँ, न बहिन न बेटी। अपनी कामवासना की पूर्ति के लिए वह कुत्तों की तरह लड़ता, झगड़ता और छीना-झपटी करता। हिन्दू धर्म के अनुसार होने वाले विवाह में प्रयोग में आने वाले मंत्रों द्वारा कन्या यह कहती है कि- ‘‘तुम कभी पर-स्त्री का चिन्तन नहीं करोंगे और मैं पति-परायण होकर तुम्हारे ही साथ निर्वाह करूँगी। तुम्हारे सिवा अन्य किसी पुरुष को पुरुष ही नहीं समझूँगी।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book