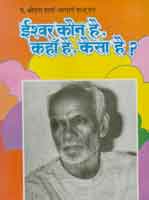|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है ?(सजिल्द) ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है ?(सजिल्द)श्रीराम शर्मा आचार्य
|
385 पाठक हैं |
||||||
ईश्वर के विषय की जानकारी....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रस्तुत वाङ़्मय एक प्रयास है, इस युग के व्यास परमपूज्य गुरुदेव पं.
श्रीराम शर्मा आचार्य के जीवन-दर्शन को जन-जन तक पहुँचाने का। आज से 85
वर्ष पूर्व आगरा के आँवलखेड़ा ग्राम में जन्मा वेदमूर्ति तपोनिष्ठ की
उपाधि प्राप्त भारतीय संस्कृति के उन्नयन को समर्पित एवं सच्चे अर्थों में
ब्राह्मणत्व को जीवन में उतारने वाला यह राष्ट्र -सन्त अपने अस्सी वर्ष के
आयुष्य में (1911-1990) आठ सौ से अधिक का कार्य कर गया। सादगी की
प्रतिमूर्ति, ममत्व, स्नेह से लबालब अंतःकरण एवं समाज की हर पीड़ा जिनकी
निज की निज की पीड़ा थी, ऐसा जीवन जीने वाले युगदृष्टा ने जीवन भर जो
लिखा, अपनी वाणी से कहा, औरों को प्रेरित कर उनसे जो संपन्न करा लिया, उस
सबको विषयानुसार इस वाङ़्मय के खण्डों में बाँधना एक नितान्त असम्भव कार्य
है। यदि यह सफल बन पड़ा है तो मात्र उस गुरुसत्ता के आशीष से ही, जिनकी हर
श्वाँस गायत्री यज्ञमय थी एवं समिधा की तरह जिनने अपने को संस्कृति -यज्ञ
में होम कर डाला।
उनकी जीवनावधि के अस्सी वर्षों में से प्रारम्भिक तीस वर्ष जन्मस्थली आँवलखेड़ा, आगरा जनपद एवं नगर में एक साधक, समाज-सुधारक, प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह बीते ! इसके बाद के तीस वर्ष मथुरा में एक विलक्षण कर्मयोगी, संगठन निर्माता, भविष्य दृष्टा, सारी मानव -जाति को एक सूत्र में पिरोकर युग निर्माण सत्संकल्प के रूप में मिशन का ‘मैनिफेस्टो’ सतयुगी समाज का आधार बताकर प्रस्तुत करते दृष्टिगोचर होते हैं। इस पूरी अवधि में एवं आयुष्य के अंतिम बीस वर्षों में परमवंदनीय माताजी का हर निमिष उनका साथ रहा। अंतिम बीस वर्ष शांतिकुंज हरिद्वार या सूक्ष्मशरीर से हिमालय में बीते। ऋषि परम्परा का बीजारोपण, सिद्ध तीर्थ गायत्री तीर्थ का निर्माण एवं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के लिए संकल्पित ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान एवं समर्थक साहित्य का लेखन इसी अवधि में हुआ। जीवन भर उनने लिखा, हर विषय को स्पर्श किया एवं जीवन मूरि की तरह भाव-संवेदना को अनुप्राणित करने वाली अपनी लेखनी साधना की। स्वयं के बारे में वे कहते थे-‘‘न हम अखबार नवीस हैं, न बुक सेलर, हम तो युगदृष्टा हैं। हमारे ये विचार क्रान्ति के बीज हैं। ये फैल गये तो सारी विश्व-वसुधा को हिलाकर रख देंगे।’’
गद्य ही नहीं, पद्य पर भी उनकी उतनी ही पकड़ थी। हजारों को प्रेरित कर उनने सृजनात्मक काव्य लिखवाया। लेखनी उनकी पन्नों के माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को बदलती चली गयी। प्रायः श्रेष्ठ लेखक, श्रेष्ठ वक्ता नहीं होते। किन्तु उनकी ओजस्वी अमृतवाणी ने लाखों का कायाकल्प कर दिया। उनके उद्बोधनों को, जो उनने भारत के कोने-कोने व मथुरा-हरिद्वार की पावन भूमि में दिए, इस वाङ्मय में देने का प्रयास किया है। करुणा छलकाती उनकी वाणी, अंतः को स्पर्श करती हुई जीवन-शैली बदलने को प्रेरित करती रहती है।
सत्तर खण्डों में जो पाँच-पाँच सौ पृष्ठ के हैं, प्रायः वह सब कुछ समा गया है, जो ऋषि युग्म के माध्यम से प्रकट हुआ। जो कमियाँ हैं, वह सम्पादन मण्डल की हैं। जो कुछ भी श्रेष्ठ है, वह सब उसी गुरु-सत्ता का है, उन्हीं का है, उन्हीं को समर्पित है।
उनकी जीवनावधि के अस्सी वर्षों में से प्रारम्भिक तीस वर्ष जन्मस्थली आँवलखेड़ा, आगरा जनपद एवं नगर में एक साधक, समाज-सुधारक, प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह बीते ! इसके बाद के तीस वर्ष मथुरा में एक विलक्षण कर्मयोगी, संगठन निर्माता, भविष्य दृष्टा, सारी मानव -जाति को एक सूत्र में पिरोकर युग निर्माण सत्संकल्प के रूप में मिशन का ‘मैनिफेस्टो’ सतयुगी समाज का आधार बताकर प्रस्तुत करते दृष्टिगोचर होते हैं। इस पूरी अवधि में एवं आयुष्य के अंतिम बीस वर्षों में परमवंदनीय माताजी का हर निमिष उनका साथ रहा। अंतिम बीस वर्ष शांतिकुंज हरिद्वार या सूक्ष्मशरीर से हिमालय में बीते। ऋषि परम्परा का बीजारोपण, सिद्ध तीर्थ गायत्री तीर्थ का निर्माण एवं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के लिए संकल्पित ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान एवं समर्थक साहित्य का लेखन इसी अवधि में हुआ। जीवन भर उनने लिखा, हर विषय को स्पर्श किया एवं जीवन मूरि की तरह भाव-संवेदना को अनुप्राणित करने वाली अपनी लेखनी साधना की। स्वयं के बारे में वे कहते थे-‘‘न हम अखबार नवीस हैं, न बुक सेलर, हम तो युगदृष्टा हैं। हमारे ये विचार क्रान्ति के बीज हैं। ये फैल गये तो सारी विश्व-वसुधा को हिलाकर रख देंगे।’’
गद्य ही नहीं, पद्य पर भी उनकी उतनी ही पकड़ थी। हजारों को प्रेरित कर उनने सृजनात्मक काव्य लिखवाया। लेखनी उनकी पन्नों के माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को बदलती चली गयी। प्रायः श्रेष्ठ लेखक, श्रेष्ठ वक्ता नहीं होते। किन्तु उनकी ओजस्वी अमृतवाणी ने लाखों का कायाकल्प कर दिया। उनके उद्बोधनों को, जो उनने भारत के कोने-कोने व मथुरा-हरिद्वार की पावन भूमि में दिए, इस वाङ्मय में देने का प्रयास किया है। करुणा छलकाती उनकी वाणी, अंतः को स्पर्श करती हुई जीवन-शैली बदलने को प्रेरित करती रहती है।
सत्तर खण्डों में जो पाँच-पाँच सौ पृष्ठ के हैं, प्रायः वह सब कुछ समा गया है, जो ऋषि युग्म के माध्यम से प्रकट हुआ। जो कमियाँ हैं, वह सम्पादन मण्डल की हैं। जो कुछ भी श्रेष्ठ है, वह सब उसी गुरु-सत्ता का है, उन्हीं का है, उन्हीं को समर्पित है।
समर्पणम्
ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामञ्ञ जगद्गुरुम्।
पादपद्मे तयो: श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुह:।।
मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका।
नामोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा-प्रज्ञा युता च या।।
भगवत्या: जगन्मातु:, श्रीरामस्य जगद्गुरो:।
पादुकायुगले वन्दे, श्रद्धाप्रज्ञास्वरूपयो:।।
नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा।
यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्।।
असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतिरोधसक्षमम्।
युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्।।
त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये।
पादपद्मे तयो: श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुह:।।
मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका।
नामोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा-प्रज्ञा युता च या।।
भगवत्या: जगन्मातु:, श्रीरामस्य जगद्गुरो:।
पादुकायुगले वन्दे, श्रद्धाप्रज्ञास्वरूपयो:।।
नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा।
यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्।।
असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतिरोधसक्षमम्।
युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्।।
त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये।
भूमिका
ईश्वर विश्वास पर ही मानव प्रगति का इतिहास टिका हुआ है। जब यह डगमगा टिका
हुआ है। जब यह डगमगा जाता है तो व्यक्ति इधर-उधर हाथ-पाँव फेंकता
विक्षुब्ध मन:स्थिति को प्राप्त होता दिखाई देता है। ईश्वर चेतना की वह
शक्ति है जो ब्राह्मण के भीतर और बाहर जो कुछ है, उस सब में संव्याप्त है।
उसके अगणित क्रिया-कलाप हैं जिनमें एक कार्य प्रकृति का- विश्व व्यवस्था
संचालन भी है। संचालक होते हुए भी वह दिखाई नहीं देता क्योंकि वह
सर्वव्यापी सर्वनियन्ता है। इसी गुत्थी के कारण की वह दिखाई क्यों नहीं
देता, एक प्रश्न साधारण मानव के मन में उठता है- ईश्वर कौन है, कहाँ है,
कैसा है ?
परम पूज्य गुरुदेव ने मानवी अस्तित्व से जुड़े इस सबसे अहम् प्रश्न, जो आस्तिकता की धुरी भी है, का जवाब देते हुए वाङ्मय के इस खण्ड में विज्ञान व शास्त्रों की कसौटी पर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया है। मात्र स्रष्टि संचालन ही ईश्वर का काम नहीं है चूंकि हमारा संबंध उसके साथ इसी सीमा तक है, अपनी मान्यता यही है कि वह इसी क्रिया-प्रक्रिया में निरत रहता होगा, अत: उसे दिखाई भी देना चाहिए। मनुष्य की यह आकांक्षा एक बाल कौतुक ही कही जानी चाहिए क्योंकि अचिन्त्य, अगोचर, अगम्य परमात्मा-पर ब्रह्म-ब्राह्मी चेतना के रूप में अपने ऐश्वर्यशाली रूप में सारे ब्रह्माण में, इको सिस्टम के कण-कण में संव्याप्त है।
ईश्वर कैसा है कौन है, यह जानने के लिए हमें उसे सबसे पहले आत्मविश्वास-सुदृढ़ आत्म-श्रेष्ठताओं का रूप अपने भीतर ही खोजना होगा। परमपूज्य गुरुदेव का ईश्वर सद्गुणों को उतारता चला जाता है, वह उतना ही ईश्वरत्व से अभिपूरित होता चला जाता है। ईश्वर तत्त्व की-आस्तिकता की यह परिभाषा अपने आप में अनूठी है एवं पूज्यवर की ही अपने ऋषि प्रणीत शैली में लिखी गयी है। उनकी लालित्यपूर्ण भाषा में ईश्वर ‘‘रसो वैसै:’’ के रूप में भी विद्यमान है तथा वेदान्त के तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म के रूप में भी। व्यक्तित्व के स्तर को ‘‘जीवो ब्रह्मै व नापर:’’ की उक्ति के अनुसार ईश्वर दर्शन है-आत्म साक्षात्कार है- जीवन्मुक्त स्थिति है।
एक जटिल तत्त्व दर्शन जिसमें नास्तिकता का प्रतिपादन करने वाले एक-एक तथ्य की काट की गयी है, को कैसे सरस बनाकर व्यक्ति को आस्तिकता मानने पर विवश कर दिया जाय, यह विज्ञ जन वाङ्मय के इस खण्ड को पढ़कर अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर के संबंध में भ्रान्तियाँ भी कम नहीं हैं। बालबुद्धि के लोग कशाय कल्मशों को धोकर साधना के राजमार्ग पर चलने को एक झंझट मानकर सस्ती पगडण्डी का मार्ग खोजते हैं। उन्हें वही शार्टकट पसंद आता है। वे सोचते हैं कि दृष्टिकोण को घटिया बनाए रखकर भी थोड़ी बहुत पूजा-उपचार करके ईश्वर को प्रसन्न भी किया जा सकता है व ईश्वर विश्वास का दिखावा भी। जब कि ऐसा नहीं है। परमपूज्य गुरुदेव उपासना, साधना, आराधाना की त्रिविध राह पर चल कर ही ईश्वर दर्शन संभव है यह समझाते हैं व तत्त्व-दर्शन के साथ-साथ व्यावहारिक समाधान भी देते हैं।
ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है-यह जान लेने पर, वह भी रोजमर्रा के उदाहरणों से; एवं विज्ञान सम्मत शैली द्वारा समझ लेने पर किसी को भी कोई संशय नहीं रह जाता कि आस्तिकता का तत्त्व दर्शन ही सही है। चार्वाकवादी नास्तिकता परक मान्यताएँ नहीं। यह इसलिए भी जरुरी है कि ईश्वर विश्वास यदि धरती पर नहीं होगा तो समाज में अनीति मूलक मान्यताओं वर्जनाओं को लांघकर किये गए दुष्कर्मो का ही बाहुल्य चारों और होगा, कर्मफल से फिर कोई डरेगा नहीं और चारों और नरपशु, नरकीटकों का या जिसकी लाठी उसकी भैंस का शासन नजर आएगा। अपने कर्मों के प्रति व्यक्ति सजग रहे, इसीलिए ईश्वर विश्वास जरूरी है। कर्मों के फल को उसी को अर्पण कर उसी के निमित्त मनुष्य कार्य करता रहे, यही ईश्वर की इच्छा है जो गीताकार ने भी समझाई है।
ईश्वर शब्द बड़ा अभिव्यंजनात्मक है। सारी स्रष्टि में जिसका एश्वर्य छाया पड़ा हो, चारों ओर जिसका सौंदर्य दिखाई देता हो-स्रष्टि के हर कण में उसकी झाँकी देखी जा सकती हो, वह कितना ऐश्वर्यशाली होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए उसे अचिन्तय बताया गया है। इस सृष्टि में यदि को हर वस्तु का कोई निमित्तकारण है-कर्ता है तो वह ईश्वर है। वह बाजीगर की तरह अपनी सारी कठपुतलियों को नचाया करता है व ऊपर से बैठकर तमाशा देखता रहता है। यही पर ब्रह्म ब्राह्मी चेतना, जिसे हर श्वास में हर कार्य में, हर पल अनुभव किया जा सकता है-सही अर्थों मे ईश्वर है। प्राणों के समुच्चय को जिस प्रकार महाप्राण कहते हैं, ऐसे ही आत्माओं के समुच्चय को सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट रूप को हम सब के परमपिता को परमात्मा कहते हैं। ईश्वर के संबंध में एक गूढ़ विवेचन का सरल सुबोध प्रतिपादन हर पाठक परिजन को संतुष्ट के उसे सही अर्थों में आस्तित्व बनाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है।
परम पूज्य गुरुदेव ने मानवी अस्तित्व से जुड़े इस सबसे अहम् प्रश्न, जो आस्तिकता की धुरी भी है, का जवाब देते हुए वाङ्मय के इस खण्ड में विज्ञान व शास्त्रों की कसौटी पर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया है। मात्र स्रष्टि संचालन ही ईश्वर का काम नहीं है चूंकि हमारा संबंध उसके साथ इसी सीमा तक है, अपनी मान्यता यही है कि वह इसी क्रिया-प्रक्रिया में निरत रहता होगा, अत: उसे दिखाई भी देना चाहिए। मनुष्य की यह आकांक्षा एक बाल कौतुक ही कही जानी चाहिए क्योंकि अचिन्त्य, अगोचर, अगम्य परमात्मा-पर ब्रह्म-ब्राह्मी चेतना के रूप में अपने ऐश्वर्यशाली रूप में सारे ब्रह्माण में, इको सिस्टम के कण-कण में संव्याप्त है।
ईश्वर कैसा है कौन है, यह जानने के लिए हमें उसे सबसे पहले आत्मविश्वास-सुदृढ़ आत्म-श्रेष्ठताओं का रूप अपने भीतर ही खोजना होगा। परमपूज्य गुरुदेव का ईश्वर सद्गुणों को उतारता चला जाता है, वह उतना ही ईश्वरत्व से अभिपूरित होता चला जाता है। ईश्वर तत्त्व की-आस्तिकता की यह परिभाषा अपने आप में अनूठी है एवं पूज्यवर की ही अपने ऋषि प्रणीत शैली में लिखी गयी है। उनकी लालित्यपूर्ण भाषा में ईश्वर ‘‘रसो वैसै:’’ के रूप में भी विद्यमान है तथा वेदान्त के तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म के रूप में भी। व्यक्तित्व के स्तर को ‘‘जीवो ब्रह्मै व नापर:’’ की उक्ति के अनुसार ईश्वर दर्शन है-आत्म साक्षात्कार है- जीवन्मुक्त स्थिति है।
एक जटिल तत्त्व दर्शन जिसमें नास्तिकता का प्रतिपादन करने वाले एक-एक तथ्य की काट की गयी है, को कैसे सरस बनाकर व्यक्ति को आस्तिकता मानने पर विवश कर दिया जाय, यह विज्ञ जन वाङ्मय के इस खण्ड को पढ़कर अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर के संबंध में भ्रान्तियाँ भी कम नहीं हैं। बालबुद्धि के लोग कशाय कल्मशों को धोकर साधना के राजमार्ग पर चलने को एक झंझट मानकर सस्ती पगडण्डी का मार्ग खोजते हैं। उन्हें वही शार्टकट पसंद आता है। वे सोचते हैं कि दृष्टिकोण को घटिया बनाए रखकर भी थोड़ी बहुत पूजा-उपचार करके ईश्वर को प्रसन्न भी किया जा सकता है व ईश्वर विश्वास का दिखावा भी। जब कि ऐसा नहीं है। परमपूज्य गुरुदेव उपासना, साधना, आराधाना की त्रिविध राह पर चल कर ही ईश्वर दर्शन संभव है यह समझाते हैं व तत्त्व-दर्शन के साथ-साथ व्यावहारिक समाधान भी देते हैं।
ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है-यह जान लेने पर, वह भी रोजमर्रा के उदाहरणों से; एवं विज्ञान सम्मत शैली द्वारा समझ लेने पर किसी को भी कोई संशय नहीं रह जाता कि आस्तिकता का तत्त्व दर्शन ही सही है। चार्वाकवादी नास्तिकता परक मान्यताएँ नहीं। यह इसलिए भी जरुरी है कि ईश्वर विश्वास यदि धरती पर नहीं होगा तो समाज में अनीति मूलक मान्यताओं वर्जनाओं को लांघकर किये गए दुष्कर्मो का ही बाहुल्य चारों और होगा, कर्मफल से फिर कोई डरेगा नहीं और चारों और नरपशु, नरकीटकों का या जिसकी लाठी उसकी भैंस का शासन नजर आएगा। अपने कर्मों के प्रति व्यक्ति सजग रहे, इसीलिए ईश्वर विश्वास जरूरी है। कर्मों के फल को उसी को अर्पण कर उसी के निमित्त मनुष्य कार्य करता रहे, यही ईश्वर की इच्छा है जो गीताकार ने भी समझाई है।
ईश्वर शब्द बड़ा अभिव्यंजनात्मक है। सारी स्रष्टि में जिसका एश्वर्य छाया पड़ा हो, चारों ओर जिसका सौंदर्य दिखाई देता हो-स्रष्टि के हर कण में उसकी झाँकी देखी जा सकती हो, वह कितना ऐश्वर्यशाली होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए उसे अचिन्तय बताया गया है। इस सृष्टि में यदि को हर वस्तु का कोई निमित्तकारण है-कर्ता है तो वह ईश्वर है। वह बाजीगर की तरह अपनी सारी कठपुतलियों को नचाया करता है व ऊपर से बैठकर तमाशा देखता रहता है। यही पर ब्रह्म ब्राह्मी चेतना, जिसे हर श्वास में हर कार्य में, हर पल अनुभव किया जा सकता है-सही अर्थों मे ईश्वर है। प्राणों के समुच्चय को जिस प्रकार महाप्राण कहते हैं, ऐसे ही आत्माओं के समुच्चय को सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट रूप को हम सब के परमपिता को परमात्मा कहते हैं। ईश्वर के संबंध में एक गूढ़ विवेचन का सरल सुबोध प्रतिपादन हर पाठक परिजन को संतुष्ट के उसे सही अर्थों में आस्तित्व बनाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है।
ब्रह्मवर्चस
आस्तिकता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी
विश्व का सर्वोत्कृष्ट दर्शन आस्तिकवाद
आस्तिकता का अर्थ और स्वरूप गहराई से न समझ सकने वाले संसार के कतिपय
समाजों ने उसे एक निरर्थक ईश्वरवाद मानकर अपने से बहिष्कृत कर नये नैतिक
स्वरूप का प्रवर्तन किया और आशा की कि इस प्रकार अपने समाज में स्थायी
सुख-शांति और सामान्य सदाचार को मूर्तिमान करने में सफल हो सकेंगे। किन्तु
उनकी यह आशा पूरी होती नहीं दिखलाई दी।
इस नये प्रयोग को समाजवाद, राष्ट्रवाद अथवा साम्यवाद के नाम से पुकारा गया और कहा गया कि यदि समाज के लोग अपनी निष्ठा को न दिखने वाले ईश्वर की ओर से हटाकर इन यथार्थवादों में लगायें, तो समाज में स्थायी सुख-शान्ति की स्थापना हो सकती है। पिछले पचपन-पचास वर्ष से इस नई विचारधारा का परीक्षण एवं प्रयोग साम्यवादी कहे जाने वाले देशों में होता चला आ रहा है। किन्तु उसका परिणाम देखते हुये यही मानने पर मजबूर होना पड़ता है कि यह प्रयोग सफलता से आभूषित न हो सका। उदाहरण के लिए साम्यवाद की मूलभूमि रूप को ही ले लिया जाय और देखा जाय कि क्या उसका समाज अपनी नवीन अवस्थाओं के आधार पर अपने जन-समूह के लिये वह वांछित सुख-शान्ति अर्जित कर सका है, जिसके लोभ से उसने उनका प्रवर्तन किया था ?
राष्ट्रवाद और समाजवाद का भरपूर शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने के बावजूद भी क्या उसके समाज में वह मानवीय सदाचार प्रौढ़ हो सका है, जो सुख-शान्ति का मूल-आधार है ? यदि सच पूछा जाय तो वहाँ अपराधों की संख्या अधिक ही है, अपेक्षाकृत उन समाजों के जो अब भी आस्तिकता और ईश्वर में आस्था रखते हैं। भ्रष्टाचार मिटाने और सदाचार लाने के लिये राजदण्ड को कठोर बना दिया गया है, दुष्प्रवृत्तियाँ रोकने के लिए उत्पीड़न और रक्तपात भी कम नहीं किया जाता, तब भी मन्तव्य की सिद्धि होते नहीं दीखती।
ऊपर से देखने में तो ऐसा ही लगता है कि दमन, नियन्त्रण और प्रतिबन्धों ने जनता का हृदय परिवर्तित कर दिया है। लोग समाजवाद और राष्ट्रवाद की दुहाई भी देते हैं। भ्रष्टाचार आदि अहितकर प्रवृत्तियों के प्रति घृणा भी दिखलाते हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि लोगों में खुले-खेलने का साहस तो कम हो गया है पर भीतर-ही-भीतर अनैतिकता की आग बराबर सुलगती रहती है, जो अवसर पाकर भय और आतंक को एक ओर ठेलकर जब-तब प्रकट होती रहती है। यह तो सच्चा सुधार नहीं माना जा सकता।
दमन, दण्ड, और आतंक के भय से यदि ऊपर-ऊपर से किन्हीं सदाचारों का प्रदर्शन करते रहा जाय और भीतर ही भीतर उसे मजबूरी अथवा अत्याचार समझा जाये तो उसे सच्ची सदाचार प्रवृत्ति नहीं माना जा सकता। सच्चा सदाचरण तो तब माना जायेगा, जब वाह्य के साथ मनुष्य का हृदय भी उसे स्वीकार करे। अवसर आने पर और कोई अथवा प्रतिबन्ध न रहने पर भी लोग सहर्ष उसकी रक्षा करें। आतंक से प्रेरित मनुष्य का कोई भी गुण, गुण नहीं बल्कि एक यांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसका न कोई मूल्य है न महत्व।
इस नये प्रयोग को समाजवाद, राष्ट्रवाद अथवा साम्यवाद के नाम से पुकारा गया और कहा गया कि यदि समाज के लोग अपनी निष्ठा को न दिखने वाले ईश्वर की ओर से हटाकर इन यथार्थवादों में लगायें, तो समाज में स्थायी सुख-शान्ति की स्थापना हो सकती है। पिछले पचपन-पचास वर्ष से इस नई विचारधारा का परीक्षण एवं प्रयोग साम्यवादी कहे जाने वाले देशों में होता चला आ रहा है। किन्तु उसका परिणाम देखते हुये यही मानने पर मजबूर होना पड़ता है कि यह प्रयोग सफलता से आभूषित न हो सका। उदाहरण के लिए साम्यवाद की मूलभूमि रूप को ही ले लिया जाय और देखा जाय कि क्या उसका समाज अपनी नवीन अवस्थाओं के आधार पर अपने जन-समूह के लिये वह वांछित सुख-शान्ति अर्जित कर सका है, जिसके लोभ से उसने उनका प्रवर्तन किया था ?
राष्ट्रवाद और समाजवाद का भरपूर शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने के बावजूद भी क्या उसके समाज में वह मानवीय सदाचार प्रौढ़ हो सका है, जो सुख-शान्ति का मूल-आधार है ? यदि सच पूछा जाय तो वहाँ अपराधों की संख्या अधिक ही है, अपेक्षाकृत उन समाजों के जो अब भी आस्तिकता और ईश्वर में आस्था रखते हैं। भ्रष्टाचार मिटाने और सदाचार लाने के लिये राजदण्ड को कठोर बना दिया गया है, दुष्प्रवृत्तियाँ रोकने के लिए उत्पीड़न और रक्तपात भी कम नहीं किया जाता, तब भी मन्तव्य की सिद्धि होते नहीं दीखती।
ऊपर से देखने में तो ऐसा ही लगता है कि दमन, नियन्त्रण और प्रतिबन्धों ने जनता का हृदय परिवर्तित कर दिया है। लोग समाजवाद और राष्ट्रवाद की दुहाई भी देते हैं। भ्रष्टाचार आदि अहितकर प्रवृत्तियों के प्रति घृणा भी दिखलाते हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि लोगों में खुले-खेलने का साहस तो कम हो गया है पर भीतर-ही-भीतर अनैतिकता की आग बराबर सुलगती रहती है, जो अवसर पाकर भय और आतंक को एक ओर ठेलकर जब-तब प्रकट होती रहती है। यह तो सच्चा सुधार नहीं माना जा सकता।
दमन, दण्ड, और आतंक के भय से यदि ऊपर-ऊपर से किन्हीं सदाचारों का प्रदर्शन करते रहा जाय और भीतर ही भीतर उसे मजबूरी अथवा अत्याचार समझा जाये तो उसे सच्ची सदाचार प्रवृत्ति नहीं माना जा सकता। सच्चा सदाचरण तो तब माना जायेगा, जब वाह्य के साथ मनुष्य का हृदय भी उसे स्वीकार करे। अवसर आने पर और कोई अथवा प्रतिबन्ध न रहने पर भी लोग सहर्ष उसकी रक्षा करें। आतंक से प्रेरित मनुष्य का कोई भी गुण, गुण नहीं बल्कि एक यांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसका न कोई मूल्य है न महत्व।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book