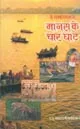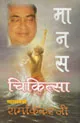|
बहुभागीय पुस्तकें >> ज्ञानदीपक द्वितीय भाग ज्ञानदीपक द्वितीय भागश्रीरामकिंकर जी महाराज
|
1 पाठक हैं |
||||||
जड़ चेतन की वास्तविकता
इस पुस्तक का सेट खरीदें।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भूमिका
भगवान शंकर के अन्त:करण की अभिव्यक्ति ही मानस है एवं उस मानस-पुण्डरीक के
मकरन्द का रसावादन करने वाले मंजुल चंचरीक हैं ‘परमपूज्य महाराजश्री
रामकिंकरजी’। पूज्य श्री रामकिंकरजी अवढ़रदानी के मानस-पुण्डरीक में
मकरंद का पान स्वत: ही नहीं करते, अपितु अनेक स्थानों पर जा-जाकर मधुरतया
गुनगुनाते हुए अपने प्रियतम की रसानुभूति सहृदय समाज को सुनाते हैं तथा
रामकथा के दिव्य रस में सहृदय समाज का आलोडन-विलोडन कराते हैं।
यदि हम स्थूल ऐतिहासिक दृष्टि से भी विचार करें तो श्रीरामचरितमानस ही श्रीरामकथा का परिष्कृततम रूप है एवं परमपूज्य महाराजश्री श्रीरामचरितमानस का दर्शन कराने के लिए मंजुलमणि हैं।
वेदान्तशास्त्र को यथार्थत: हृदयंगम कर पाना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है, परन्तु महाराजश्री के प्रवचनों को रसास्वादन करने के समनन्तर ऐसा प्रतीत होता है कि वेदान्तशास्त्र का निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में मूर्तिमान् होकर अपने रहस्यों को स्वत: उपन्यस्त कर रहा है। जीवनदर्शन एवं वेदान्तशास्त्र की सहव्याख्या गोस्वामीजी की रामकथा की महती विशिष्टता है तथा जीवनदर्शन को माध्यम बना करके वेदान्तशास्त्र के ‘रसो वै स:’ के रहस्यों को उद्धाटित करना पूज्य महाराजश्री का लक्ष्य प्रतीत होता है। यदि कोई व्यक्ति तर्क का आधार स्वीकार करते हुए रामकथा में अतिशयोक्ति का दर्शन करता है तो महाराजश्री का प्रतीकात्मक भाष्य उसकी तर्कबुद्धि के लिए औषध के समान है। महाराजश्री के भाष्यों में जब मनोवृत्तियों की तुलना मानस के पात्रों से की जाती है तो विश्वास होने लगता है कि गोस्वामीजी ने भगवान् राम के मंगलमय जीवन वर्णन के साथ-साथ ही सम्पूर्ण मनोवृत्तियों की भी पारदर्शी व्याख्या प्रस्तुत कर दी है। फलत: ऐसा सिद्ध होने लगता है कि मानस सूत्र है और पूज्य महाराजश्री मानस के भाष्य हैं।
प्रस्तुत ग्रन्थ में मानस में वर्णित ज्ञानदीपक प्रसंग को आधार बनाकर महाराजश्री द्वारा दो सत्रों में प्रोक्त सत्रह प्रवचनों का संग्रह है। सत्रहों प्रवचनों में तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के साधनों की नीर-क्षीर विवेचनापूर्ण विशद चर्चा है। ज्ञानदीपक प्रसंग जितना गंभीर है, इस ग्रंथ में उसकी व्याख्या उतनी ही सहज एवं सरल है। प्रचलित परम्परा के अनुसार सामान्यत: ऐसे विषयों पर कथा नहीं होती है, अत: रामकथा के माध्यम से तत्त्वज्ञान की चर्चा के रूप में यह दुर्लभ प्रसंग है। इस ग्रंथ का हृदयंगम करने से वह उक्ति चरितार्थ होने लगती है, जिसमें यह कहा गया है कि मानस समस्त श्रुतिसम्मत मार्गों की अद्भुत व्याख्या है।
तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के जितने साधन हैं, प्राय: वे सब प्रस्तुत ग्रंथ में मूर्तिमान होकर अपनी प्रत्यक्ष व्याख्या प्रस्तुत करते देखे जा सकते हैं। सात्त्विक श्रद्धा का स्वत:स्फूर्त निरुपण पार्वतीजी में विद्यमान है, इसी प्रकार सत्कर्म की व्याख्या पार्वतीजी तपस्या में तथा भाव का विस्तृत विवेचन महाराज मनु में रुपायित होता है, किन्तु सत्रह प्रवचनों में ही व्यासशैली में तत्त्वज्ञान के घटकों की व्याख्या संभव नहीं थी, अत: तत्त्वज्ञान की व्याख्या की समासशैली भी स्वीकृत की गयी है। फलत: मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार की दोषयुक्त स्वीकृति का पक्ष कैकेयी में तथा गुणयुक्त स्वीकृति का उज्ज्वल पक्ष श्रीभरतजी के निर्मल चरित्र में अभिव्यक्त होता है। मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार को विशुद्ध बनाने के लिए श्रीभरतजी के चरित्र की प्रेरणा साधकों के लिए कल्पतरु है, इस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप ही अखण्डज्ञानघन श्रीराम से एकत्व संभव है। एतदतिरिक्त अन्त में संत गोस्वामी द्वारा वर्णित तत्त्वज्ञान की प्राप्ति की पद्धति भी व्याख्यायित है।
प्रस्तुत ग्रन्थ सहृय एवं विज्ञ पाठकों के अन्त:करण के लिए प्रसादपूर्ण नैवेद्य हो सकता है, तथापि सावधानी की चेष्टाओं के बाद भी प्रस्तुत ग्रन्थ में सम्पादकीय त्रुटियाँ सम्भावित हैं। अत: सुधी पाठकों से क्षमा प्रार्थना पूर्वक निवेदन है कि त्रुटियों से हमें अवगत कराने की महती कृपा करें, जिससे अगले संस्करण में सुधारा जा सके।
यदि हम स्थूल ऐतिहासिक दृष्टि से भी विचार करें तो श्रीरामचरितमानस ही श्रीरामकथा का परिष्कृततम रूप है एवं परमपूज्य महाराजश्री श्रीरामचरितमानस का दर्शन कराने के लिए मंजुलमणि हैं।
वेदान्तशास्त्र को यथार्थत: हृदयंगम कर पाना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है, परन्तु महाराजश्री के प्रवचनों को रसास्वादन करने के समनन्तर ऐसा प्रतीत होता है कि वेदान्तशास्त्र का निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में मूर्तिमान् होकर अपने रहस्यों को स्वत: उपन्यस्त कर रहा है। जीवनदर्शन एवं वेदान्तशास्त्र की सहव्याख्या गोस्वामीजी की रामकथा की महती विशिष्टता है तथा जीवनदर्शन को माध्यम बना करके वेदान्तशास्त्र के ‘रसो वै स:’ के रहस्यों को उद्धाटित करना पूज्य महाराजश्री का लक्ष्य प्रतीत होता है। यदि कोई व्यक्ति तर्क का आधार स्वीकार करते हुए रामकथा में अतिशयोक्ति का दर्शन करता है तो महाराजश्री का प्रतीकात्मक भाष्य उसकी तर्कबुद्धि के लिए औषध के समान है। महाराजश्री के भाष्यों में जब मनोवृत्तियों की तुलना मानस के पात्रों से की जाती है तो विश्वास होने लगता है कि गोस्वामीजी ने भगवान् राम के मंगलमय जीवन वर्णन के साथ-साथ ही सम्पूर्ण मनोवृत्तियों की भी पारदर्शी व्याख्या प्रस्तुत कर दी है। फलत: ऐसा सिद्ध होने लगता है कि मानस सूत्र है और पूज्य महाराजश्री मानस के भाष्य हैं।
प्रस्तुत ग्रन्थ में मानस में वर्णित ज्ञानदीपक प्रसंग को आधार बनाकर महाराजश्री द्वारा दो सत्रों में प्रोक्त सत्रह प्रवचनों का संग्रह है। सत्रहों प्रवचनों में तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के साधनों की नीर-क्षीर विवेचनापूर्ण विशद चर्चा है। ज्ञानदीपक प्रसंग जितना गंभीर है, इस ग्रंथ में उसकी व्याख्या उतनी ही सहज एवं सरल है। प्रचलित परम्परा के अनुसार सामान्यत: ऐसे विषयों पर कथा नहीं होती है, अत: रामकथा के माध्यम से तत्त्वज्ञान की चर्चा के रूप में यह दुर्लभ प्रसंग है। इस ग्रंथ का हृदयंगम करने से वह उक्ति चरितार्थ होने लगती है, जिसमें यह कहा गया है कि मानस समस्त श्रुतिसम्मत मार्गों की अद्भुत व्याख्या है।
तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के जितने साधन हैं, प्राय: वे सब प्रस्तुत ग्रंथ में मूर्तिमान होकर अपनी प्रत्यक्ष व्याख्या प्रस्तुत करते देखे जा सकते हैं। सात्त्विक श्रद्धा का स्वत:स्फूर्त निरुपण पार्वतीजी में विद्यमान है, इसी प्रकार सत्कर्म की व्याख्या पार्वतीजी तपस्या में तथा भाव का विस्तृत विवेचन महाराज मनु में रुपायित होता है, किन्तु सत्रह प्रवचनों में ही व्यासशैली में तत्त्वज्ञान के घटकों की व्याख्या संभव नहीं थी, अत: तत्त्वज्ञान की व्याख्या की समासशैली भी स्वीकृत की गयी है। फलत: मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार की दोषयुक्त स्वीकृति का पक्ष कैकेयी में तथा गुणयुक्त स्वीकृति का उज्ज्वल पक्ष श्रीभरतजी के निर्मल चरित्र में अभिव्यक्त होता है। मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार को विशुद्ध बनाने के लिए श्रीभरतजी के चरित्र की प्रेरणा साधकों के लिए कल्पतरु है, इस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप ही अखण्डज्ञानघन श्रीराम से एकत्व संभव है। एतदतिरिक्त अन्त में संत गोस्वामी द्वारा वर्णित तत्त्वज्ञान की प्राप्ति की पद्धति भी व्याख्यायित है।
प्रस्तुत ग्रन्थ सहृय एवं विज्ञ पाठकों के अन्त:करण के लिए प्रसादपूर्ण नैवेद्य हो सकता है, तथापि सावधानी की चेष्टाओं के बाद भी प्रस्तुत ग्रन्थ में सम्पादकीय त्रुटियाँ सम्भावित हैं। अत: सुधी पाठकों से क्षमा प्रार्थना पूर्वक निवेदन है कि त्रुटियों से हमें अवगत कराने की महती कृपा करें, जिससे अगले संस्करण में सुधारा जा सके।
सम्पादक
गुरुपूर्णिमा (सन्-2004)
।। श्रीराम: शरणं मम ।।
प्रथम
सात्त्विक श्रद्धा धेनु सुहाई।
जौं हरि कृपाँ हृदयँ बस आई।।
जप तप ब्रत जम नियम अपारा।
जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ।।
तेई तृन हरित चरै जब गाई।
भाव बच्छ सिसु पाई पेन्हाई।।
नोइ निबृत्ति पात्र बिस्वासा।
निर्मल मन अहीर निज दासा।
परम धर्ममय पय दुहि भाई।
अवटै अनल अकाम बनाई।।
तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावै।
धृति सम जावनु देइ जमावै।।
मुदिताँ मथै बिचार मथानी।
दम अधार रजु सत्य सुबानी।।
तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता।
बिमल बिराग सुभग सुपुनीता।।
जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ।
बुद्धि सिरावै ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ।। 7/117
जौं हरि कृपाँ हृदयँ बस आई।।
जप तप ब्रत जम नियम अपारा।
जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ।।
तेई तृन हरित चरै जब गाई।
भाव बच्छ सिसु पाई पेन्हाई।।
नोइ निबृत्ति पात्र बिस्वासा।
निर्मल मन अहीर निज दासा।
परम धर्ममय पय दुहि भाई।
अवटै अनल अकाम बनाई।।
तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावै।
धृति सम जावनु देइ जमावै।।
मुदिताँ मथै बिचार मथानी।
दम अधार रजु सत्य सुबानी।।
तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता।
बिमल बिराग सुभग सुपुनीता।।
जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ।
बुद्धि सिरावै ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ।। 7/117
आइए ! एकाग्र और शान्तचित्त से इस प्रसंग को हृदयंगम करने की चेष्टा करें।
व्यक्ति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सुख की है। व्यक्ति सुख चाहता है, परन्तु न चाहते हुए भी उसके जीवन में दु:ख आ जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में इसी समस्या के समाधान के लिए एक बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। यदि आपको किसी गाँठ को सुलझाना हो तो उसके लिए प्रकाश चाहिए। यह गाँठ हमारे भीतर है, इसलिए इसे सुलझाने के लिए भीतर प्रकाश की आवश्यकता है, परन्तु हम उजाला कर रहे हैं बाहर। हमारा समस्त पुरुषार्थ केवल बाहर का अन्धकार मिटाने के लिए ही होता है। ज्ञानदीपक प्रसंग में संकेत किया गया है कि केवल बाहरी प्रकाश के लिए किसी भी प्रयत्न की आवश्यकता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक व्यक्ति स्वयं अपने अन्तर्हृदय में प्रवेश नहीं करता और वहाँ जो अन्धकार छाया हुआ है, उसको मिटाने के लिए जब तक व्यक्ति ज्ञान का दीपक नहीं जलाता, तब तक विभिन्न प्रकार के प्रयत्न केवल श्रम मात्र ही हैं।
बाहर के प्रकाश के लिए तो हम दीपक या बिजली का प्रयोग करते हैं और प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु भीतर के प्रकाश के लिए किस पद्धति से प्रकाश किया जाय, यह जानना परमआवश्यक है। ज्ञानदीपक प्रसंग में यही बताया गया है। हमारे अन्तर्हृदय में जहाँ गहरा अन्धकार छाया हुआ है, उस अन्तर्हृदय में ही दीपक जलायें और दीपक जला करके जो जड़ एवं चेतन की एक गाँठ पड़ गयी है, उसे सुलझाने की चेष्टा करें। अँधेरे में उसे सुलझाने के प्रयास में उस गाँठ के और भी उलझ जाने की संभावना है। हमारे अन्तर्हृदय में किस प्रकार प्रकाश हो, इसका वर्णन इस ज्ञानदीपक प्रसंग में किया गया है।
गोस्वामी ने इसके लिए जो साधना पद्धति बतायी है, उसकी ओर इस प्रसंग में संकेत किया गया है। वे कहते हैं कि अन्तर्हृदय के प्रकाश के लिए दीपक की आवश्यकता है और उस दीपक में जो घी हो, वह गाय के दूध से बना शुद्ध घृत होना चाहिए। क्या तेल अथवा भैंस के घी का दीपक यदि जलायें तो क्या प्रकाश नहीं होगा ? गोस्वामीजी ने गाय के घी के दीपक के लिए जो आग्रह किया है, उसका सांकेतिक अर्थ क्या है ? बुद्धि को प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। बुद्धिमत्ता तो अनगिनत व्यक्तियों में देखी जाती है, केवल बुद्धि की चमक से ही अन्तर्हृदय में प्रकाश हो जायगा यह संभव नहीं।
मानो यहाँ यह सूत्र दिया गया है कि केवल बुद्धि की ही नहीं, अपितु पवित्र बुद्धि की आवश्यकता है और पवित्रता का प्रतीक हम गाय को मानते हैं। इसलिए यहाँ पर एक क्रम का वर्णन किया गया है कि पहले जब व्यक्ति पर भगवान् की कृपा होती है तो उसके अन्त:करण में सात्त्विक श्रद्धा का उदय होता है और सात्त्विक श्रद्धा ही मानो गाय है। जैसे कितनी भी अच्छी गाय हो, जब तक उसे चारा नहीं खिलायेंगे, तब तक वह दूध नहीं देगी, उसी प्रकार से श्रद्धा होते हुए भी जब तक हमारे जीवन में सत्कर्म नहीं होगा, तब तक गाय दूध देने में समर्थ नहीं होगी तो यह कहा गया है कि सात्त्विक श्रद्धा चाहिए, उसको सत्कर्म का चारा खिलाने की आवश्यकता है और फिर इसके बाद बछड़ा चाहिए, तो कहा गया कि साधक के हृदय में जो भाव है, वही इस सात्त्विक श्रद्धा का बछड़ा है।
व्यक्ति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सुख की है। व्यक्ति सुख चाहता है, परन्तु न चाहते हुए भी उसके जीवन में दु:ख आ जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में इसी समस्या के समाधान के लिए एक बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। यदि आपको किसी गाँठ को सुलझाना हो तो उसके लिए प्रकाश चाहिए। यह गाँठ हमारे भीतर है, इसलिए इसे सुलझाने के लिए भीतर प्रकाश की आवश्यकता है, परन्तु हम उजाला कर रहे हैं बाहर। हमारा समस्त पुरुषार्थ केवल बाहर का अन्धकार मिटाने के लिए ही होता है। ज्ञानदीपक प्रसंग में संकेत किया गया है कि केवल बाहरी प्रकाश के लिए किसी भी प्रयत्न की आवश्यकता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक व्यक्ति स्वयं अपने अन्तर्हृदय में प्रवेश नहीं करता और वहाँ जो अन्धकार छाया हुआ है, उसको मिटाने के लिए जब तक व्यक्ति ज्ञान का दीपक नहीं जलाता, तब तक विभिन्न प्रकार के प्रयत्न केवल श्रम मात्र ही हैं।
बाहर के प्रकाश के लिए तो हम दीपक या बिजली का प्रयोग करते हैं और प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु भीतर के प्रकाश के लिए किस पद्धति से प्रकाश किया जाय, यह जानना परमआवश्यक है। ज्ञानदीपक प्रसंग में यही बताया गया है। हमारे अन्तर्हृदय में जहाँ गहरा अन्धकार छाया हुआ है, उस अन्तर्हृदय में ही दीपक जलायें और दीपक जला करके जो जड़ एवं चेतन की एक गाँठ पड़ गयी है, उसे सुलझाने की चेष्टा करें। अँधेरे में उसे सुलझाने के प्रयास में उस गाँठ के और भी उलझ जाने की संभावना है। हमारे अन्तर्हृदय में किस प्रकार प्रकाश हो, इसका वर्णन इस ज्ञानदीपक प्रसंग में किया गया है।
गोस्वामी ने इसके लिए जो साधना पद्धति बतायी है, उसकी ओर इस प्रसंग में संकेत किया गया है। वे कहते हैं कि अन्तर्हृदय के प्रकाश के लिए दीपक की आवश्यकता है और उस दीपक में जो घी हो, वह गाय के दूध से बना शुद्ध घृत होना चाहिए। क्या तेल अथवा भैंस के घी का दीपक यदि जलायें तो क्या प्रकाश नहीं होगा ? गोस्वामीजी ने गाय के घी के दीपक के लिए जो आग्रह किया है, उसका सांकेतिक अर्थ क्या है ? बुद्धि को प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। बुद्धिमत्ता तो अनगिनत व्यक्तियों में देखी जाती है, केवल बुद्धि की चमक से ही अन्तर्हृदय में प्रकाश हो जायगा यह संभव नहीं।
मानो यहाँ यह सूत्र दिया गया है कि केवल बुद्धि की ही नहीं, अपितु पवित्र बुद्धि की आवश्यकता है और पवित्रता का प्रतीक हम गाय को मानते हैं। इसलिए यहाँ पर एक क्रम का वर्णन किया गया है कि पहले जब व्यक्ति पर भगवान् की कृपा होती है तो उसके अन्त:करण में सात्त्विक श्रद्धा का उदय होता है और सात्त्विक श्रद्धा ही मानो गाय है। जैसे कितनी भी अच्छी गाय हो, जब तक उसे चारा नहीं खिलायेंगे, तब तक वह दूध नहीं देगी, उसी प्रकार से श्रद्धा होते हुए भी जब तक हमारे जीवन में सत्कर्म नहीं होगा, तब तक गाय दूध देने में समर्थ नहीं होगी तो यह कहा गया है कि सात्त्विक श्रद्धा चाहिए, उसको सत्कर्म का चारा खिलाने की आवश्यकता है और फिर इसके बाद बछड़ा चाहिए, तो कहा गया कि साधक के हृदय में जो भाव है, वही इस सात्त्विक श्रद्धा का बछड़ा है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book