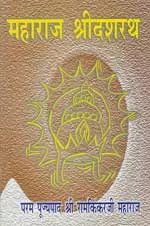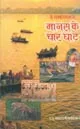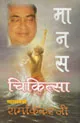|
आचार्य श्रीराम किंकर जी >> महाराज श्रीदशरथ महाराज श्रीदशरथश्रीरामकिंकर जी महाराज
|
171 पाठक हैं |
||||||
महाराज श्रीदशरथ का चरित्र-चित्रण
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
महाराज दशरथ का वर्णन आप ‘मानस’ में पढ़ते हैं, पर यदि आप यह
जानना चाहें कि महाराज दशरथ किसके पुत्र थे’ तो इसका पता, आपको
‘मानस’ से नहीं चल पाएगा किसी अन्य ग्रन्थ में खोजना पड़ेगा।
इसी तरह जनकनंदिनी श्री किशोरीजी के पूर्व-पुरुषों के नाम भी रामायण से
प्राप्त नहीं होते। स्मरण आता है, एक बार एक सज्जन ने मुझसे पूछा था कि
‘रावण के नाना के नाना का क्या नाम था ? मैंने उनसे कहा कि मुझे
तो
रावण के नाना का ही नाम मालूम नहीं, नाना के नाना के नाम की बात क्या
करूँ। पुराणों में जब हम वंश-परम्परा को पढ़ते हैं, तो उसके द्वारा हमें
इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है।
संयोजकीय
रामकथा शिरोमणि सद्गुरुदेव परमपूज्य श्री रामकिंकर जी महाराज की वाणी और
लेखनी दोनों में यह निर्णय कर पाना कठिन है कि अधिक हृदयस्पर्शी या
तात्विक कौन है। वे विषयवस्तु का समय, समाज एवं व्यक्ति की पात्रता को
आँकते हुए ऐसा विलक्षण प्रतिपादन करते हैं कि ज्ञानी, भक्त या कर्मपराण
सभी प्रकार के जिज्ञासुओं को उनकी मान्यता के अनुसार श्रेय और प्रेय दोनों
की प्राप्ति हो जाती है।
हमारे यहाँ विस्तार और संक्षेप, व्यास और समास दोनों ही विधाओं के समयानुकूल उपयोग की परम्परा रही है। घटाकाश और मटाकाश दोनों ही चिंतन और प्रतिपादन के केन्द्र रहे हैं। प्रवचनों के प्रस्तुत छोटे अंक घटाकाश के रूप में हैं, उनमें सब कुछ है पर संक्षेप में है। पाठकों की कई बार ऐसी राय बनी कि थोड़ा साहित्य छोटे रूप में भी हो ताकि प्रारम्भिक रूप में या फिर यात्रा आदि में लोग किसी एक विषय का अध्ययन करने के लिए उसे साथ लेकर चल सकें। इस मनोधारणा से यह कार्य श्रेयस्कर है।
रायपुर (छत्तीसगढ़) के श्री अनिल गुप्ता एवं समस्त परिवार का आर्थिक सहयोग इसमें सन्निहित है। उन्हें महाराजश्री का आशीर्वाद !
हमारे यहाँ विस्तार और संक्षेप, व्यास और समास दोनों ही विधाओं के समयानुकूल उपयोग की परम्परा रही है। घटाकाश और मटाकाश दोनों ही चिंतन और प्रतिपादन के केन्द्र रहे हैं। प्रवचनों के प्रस्तुत छोटे अंक घटाकाश के रूप में हैं, उनमें सब कुछ है पर संक्षेप में है। पाठकों की कई बार ऐसी राय बनी कि थोड़ा साहित्य छोटे रूप में भी हो ताकि प्रारम्भिक रूप में या फिर यात्रा आदि में लोग किसी एक विषय का अध्ययन करने के लिए उसे साथ लेकर चल सकें। इस मनोधारणा से यह कार्य श्रेयस्कर है।
रायपुर (छत्तीसगढ़) के श्री अनिल गुप्ता एवं समस्त परिवार का आर्थिक सहयोग इसमें सन्निहित है। उन्हें महाराजश्री का आशीर्वाद !
मैथिलीशरण
कृतज्ञता ज्ञापन
श्रीसद्गुरवै नमः
हमारे परिवार के आध्यात्मिक-प्रेरणास्रोत पूज्यपिताश्री नारायण प्रसाद
गुप्तजी (आरंग वाले) दिनांक 13-11-96 को अपने दिव्य धाम के लिए प्रस्थान
कर गये। उन्हीं धार्मिक विचारों से प्रेरित परिवार को इस कार्य द्वारा
माता सरस्वती के मन्दिर में एक दिव्य सुमनांजलि समर्पित करने का पुण्य
अवसर मिला। इस सबके पीछे सद्गुरु महाराजजी की कृपा एवं ईश्वरेच्छा ही मूल
कारण है। उस परम शक्तिमान के प्रति हम सदैव श्रद्धानत हैं।
यहाँ पर भाई मैथिलीशरणजी एवं परम विदुषी दीदी मंदाकिनीजी जो श्री सद्गुरुदेव के अत्यन्त प्रेमी एवं निकट हैं तथा उन सभी श्रद्धालुओं के प्रति हार्दिक धन्यवाद देना हमारा परम कर्त्तव्य है जिनका इस पुस्तक-माला में, श्रीगुरुदेव के प्रवचनों के संयोजन में, विशेष सहयोग रहा है। वे इसलिए भी धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्हीं के सहयोग और श्रद्धाभावना से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ज्ञान, आनन्द, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, दया, मैत्री, सरलता, साधुता, समता, सत्य, क्षमा आदि दैवी गुणों के विपुल भण्डार से समय-समय पर ग्रन्थ के रूप में सुलभ कराते हैं।
श्रीराम में हमारी अखण्ड भक्ति बनी रहे,
श्रीसद्गुरुदेव की कृपा सब पर वर्षित हो।
यहाँ पर भाई मैथिलीशरणजी एवं परम विदुषी दीदी मंदाकिनीजी जो श्री सद्गुरुदेव के अत्यन्त प्रेमी एवं निकट हैं तथा उन सभी श्रद्धालुओं के प्रति हार्दिक धन्यवाद देना हमारा परम कर्त्तव्य है जिनका इस पुस्तक-माला में, श्रीगुरुदेव के प्रवचनों के संयोजन में, विशेष सहयोग रहा है। वे इसलिए भी धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्हीं के सहयोग और श्रद्धाभावना से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ज्ञान, आनन्द, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, दया, मैत्री, सरलता, साधुता, समता, सत्य, क्षमा आदि दैवी गुणों के विपुल भण्डार से समय-समय पर ग्रन्थ के रूप में सुलभ कराते हैं।
श्रीराम में हमारी अखण्ड भक्ति बनी रहे,
श्रीसद्गुरुदेव की कृपा सब पर वर्षित हो।
महाराज श्रीदशरथ
सोचनीय सबहीं बिधि सोई।
जो न छाड़ि छलु हरि जन होई।।
सोचनीय नहिं कोसलराऊ।
भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ।।
भयउ न अहइ न अब होनिहारा।
भूप भरत जस पिता तुम्हारा।। 2/172/4-6
जो न छाड़ि छलु हरि जन होई।।
सोचनीय नहिं कोसलराऊ।
भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ।।
भयउ न अहइ न अब होनिहारा।
भूप भरत जस पिता तुम्हारा।। 2/172/4-6
महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद श्रीभरत का जब अयोध्या में आगमन होता है तब
गुरु वशिष्ठ जी ने भरतजी को मुख्य श्रोता बनाकर सभा में जो प्रेरक सन्देश
दिया उसी को मैं प्रस्तुत करने की चेष्टा करूँगा। यह प्रसंग उस समय का है
जब श्रीदशरथजी के प्राणत्याग के कारण शोक के वातावरण में समाये गुरु
वशिष्ठ ज्ञानमय और वैराग्यमय सन्देश देते हैं और कहते हैं कि भरत !
वस्तुतः शोक तो उन व्यक्तियों के लिए किया जाना चाहिए जिन्होंने सार्थक
जीवन न जिया हो, जिनके भविष्य के विषय में हमारे मन में आशंका हो कि पता
नहीं मृत्यु के पश्चात उनकी क्या गति हुई होगी ? यदि हम उनके लिए आँसू
बहायें, दुःखी हों तो स्वाभाविक है, पर जिन्होंने सार्थक जीवन जिया है,
उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और
उनके सूत्रों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें।
एक दृष्टि से रामकथा ऐतिहासिक है तो दूसरी दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो रामकथा जीवन का शाश्वत सत्य है। एक ओर तो यह त्रेतायुग का चित्र है और दूसरी ओर यदि हम भूतकाल को देखते हैं और दर्पण में वर्तमान को देखते हैं तो ये दोनों ही रूप बड़े उपादेय हैं, प्रेरक हैं। हम रामकथा के दर्पणात्मक रूप की ओर विशेष ध्यान दें, ऐसा मैं चाहूँगा क्योंकि उसका हमारे जीवन से बड़ा निकट का सम्बन्ध है। दशरथ की गाथा एक इतिहास-पुरुष की गाथा तो है ही, पर रामकथा में हमारे जीवन-क्रम की दो गाथाओं की ओर संकेत किया गया है।
दशरथजी पूर्व जन्म में मनु थे। उन्होंने बड़ा सार्थक जीवन जिया और अन्त में श्रीराम के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया, पर यह गाथा दो समानान्तर गाथाओं से जुड़ी हुई है। एक यात्रा है मनुष्य के दशरथ बनने की और दूसरी यात्रा है मनुष्य के दशमुख बनने की। मनुजी अगले जन्म में दशरथ बने और प्रतापभानु दशमुख बना। हम यह देखने की चेष्टा करें कि हम महाराज श्रीदशरथ के आदर्शों पर चलकर दशरथ बनने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारे सारे प्रयत्न हमें दशमुखत्व की ओर ले जा रहे हैं।
मनुष्य शब्द मनु से बना है। मनुजी मनुष्य जाति के आदि पुरुष हैं। मनु का दशरथ बनना मानों सारी मनुष्य जाति की यात्रा है कि यदि हम मनु की पद्धति से चलेंगे तो हम दशरथ बनेंगे। दूसरी ओर दशमुख बनने की यात्रा है। आप किसी ग्रन्थ में यह नहीं पायेंगे कि दशमुख बनने वाला व्यक्ति मूलतः बुरा था। बल्कि आप दोनों में सत्यता पायेंगे।
सत्यकेतु नाम के केकय देश के राजा थे और उनके दो पुत्र थे, प्रतापभानु और अरिमर्दन। ये दोनों भाई बड़े धर्मात्मा थे। उनका जीवन बड़ा पवित्र था। दूसरी ओर मनु का जीवन भी बड़ा पवित्र है। संसार के जितने जीव हैं, वे मूलतः अच्छे हैं कि बुरे हैं ? कुछ लोगों की धारणा यह है कि व्यक्ति मूलतः बुरा है, पर प्रयत्न के द्वारा उसे अच्छा बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए, पर हमारी आध्यात्मिक धारणा इससे भिन्न है। एक धारणा भौतिक विज्ञान की है, जिसकी मान्यता है कि सृष्टि में क्रमशः विकास हो रहा है, मनुष्य मूलतः पशु था। धीरे-धीरे विकास होने पर मनुष्य बना। यह विकासवाद का सिद्धान्त है। सृष्टि के मूल में जड़ है और जड़ ज्यों-ज्यों विकसित होती है, त्यों-त्यों उसकी उन्नति होती है। आध्यात्मिक धारणा इससे बिलकुल भिन्न है और उसकी मान्यता है कि सृष्टि के मूल में ईश्वर है और वह तो चैतन्य है। गोस्वामीजी ने सृष्टि के लिए जो शब्द चुना वह बड़े महत्त्व का है—
एक दृष्टि से रामकथा ऐतिहासिक है तो दूसरी दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो रामकथा जीवन का शाश्वत सत्य है। एक ओर तो यह त्रेतायुग का चित्र है और दूसरी ओर यदि हम भूतकाल को देखते हैं और दर्पण में वर्तमान को देखते हैं तो ये दोनों ही रूप बड़े उपादेय हैं, प्रेरक हैं। हम रामकथा के दर्पणात्मक रूप की ओर विशेष ध्यान दें, ऐसा मैं चाहूँगा क्योंकि उसका हमारे जीवन से बड़ा निकट का सम्बन्ध है। दशरथ की गाथा एक इतिहास-पुरुष की गाथा तो है ही, पर रामकथा में हमारे जीवन-क्रम की दो गाथाओं की ओर संकेत किया गया है।
दशरथजी पूर्व जन्म में मनु थे। उन्होंने बड़ा सार्थक जीवन जिया और अन्त में श्रीराम के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया, पर यह गाथा दो समानान्तर गाथाओं से जुड़ी हुई है। एक यात्रा है मनुष्य के दशरथ बनने की और दूसरी यात्रा है मनुष्य के दशमुख बनने की। मनुजी अगले जन्म में दशरथ बने और प्रतापभानु दशमुख बना। हम यह देखने की चेष्टा करें कि हम महाराज श्रीदशरथ के आदर्शों पर चलकर दशरथ बनने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारे सारे प्रयत्न हमें दशमुखत्व की ओर ले जा रहे हैं।
मनुष्य शब्द मनु से बना है। मनुजी मनुष्य जाति के आदि पुरुष हैं। मनु का दशरथ बनना मानों सारी मनुष्य जाति की यात्रा है कि यदि हम मनु की पद्धति से चलेंगे तो हम दशरथ बनेंगे। दूसरी ओर दशमुख बनने की यात्रा है। आप किसी ग्रन्थ में यह नहीं पायेंगे कि दशमुख बनने वाला व्यक्ति मूलतः बुरा था। बल्कि आप दोनों में सत्यता पायेंगे।
सत्यकेतु नाम के केकय देश के राजा थे और उनके दो पुत्र थे, प्रतापभानु और अरिमर्दन। ये दोनों भाई बड़े धर्मात्मा थे। उनका जीवन बड़ा पवित्र था। दूसरी ओर मनु का जीवन भी बड़ा पवित्र है। संसार के जितने जीव हैं, वे मूलतः अच्छे हैं कि बुरे हैं ? कुछ लोगों की धारणा यह है कि व्यक्ति मूलतः बुरा है, पर प्रयत्न के द्वारा उसे अच्छा बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए, पर हमारी आध्यात्मिक धारणा इससे भिन्न है। एक धारणा भौतिक विज्ञान की है, जिसकी मान्यता है कि सृष्टि में क्रमशः विकास हो रहा है, मनुष्य मूलतः पशु था। धीरे-धीरे विकास होने पर मनुष्य बना। यह विकासवाद का सिद्धान्त है। सृष्टि के मूल में जड़ है और जड़ ज्यों-ज्यों विकसित होती है, त्यों-त्यों उसकी उन्नति होती है। आध्यात्मिक धारणा इससे बिलकुल भिन्न है और उसकी मान्यता है कि सृष्टि के मूल में ईश्वर है और वह तो चैतन्य है। गोस्वामीजी ने सृष्टि के लिए जो शब्द चुना वह बड़े महत्त्व का है—
तुलसिदास कह चिद-बिलास जग जूझत बूझत बूझै।
विनय-पत्रिका, 124/5
विनय-पत्रिका, 124/5
भौतिक विज्ञान यह है कि सृष्टि जड़ का विकास है और आध्यात्मवाद का कहना है
कि सृष्टि चेतन का विलास है। ‘मानस’ में आप पढ़ेंगे
कि जीव
ईश्वर का अंश है और इस नाते ईश्वर की दिव्यता, ईश्वर का गुण ही जीव में भी
अंश रूप से विद्यमान है—
ईस्वर अंस जीव अबिनासी।
चेतन अमल सहज सुख रासी।। 7/116/2
चेतन अमल सहज सुख रासी।। 7/116/2
हम मूलतः तो चैतन्य के विलास हैं, ईश्वर के अंश हैं, पर हमने अपने आपको
मलिन बना डाला है, अपवित्र बना डाला है। वस्तुतः हम मूलतः बुरे नहीं हैं।
दशरथ और दशमुख इन दोनों के मूल में जो पूर्व जन्म के पात्र हैं उनका
चरित्र परम पवित्र था, पर अगले जन्म में परिवर्तन होता है। मनु दशरथ बन
जाते हैं और सत्यकेतु राजा के पुत्र प्रतापभानु दशमुख। प्रतापभानु शब्द का
अर्थ है कि सूर्य जैसा प्रताप या प्रकाश जिसमें विद्यमान हो। प्रतापभानु
दशमुख हो गया, निशाचर हो गया। निशाचर उसको कहते हैं जिसकी शक्ति रात्रि
में बढ़ती है, जिसे अन्धकार प्रिय है। प्रकाश अन्धकार के रूप में
परिवर्तित हो गया।
हम मूलतः ईश्वर के अंश होने से परम पवित्र हैं, परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि हम क्या बनने की चेष्टा कर रहे हैं ? दशरथ या दशमुख ? हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। दशरथ बनने की दिशा में कि दशमुख बनने की दिशा में। मनु बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने अपनी प्रजा को भी धर्मानुकूल चलाने की चेष्टा की, पर मनु को ऐसा लगा कि केवल धर्म के द्वारा जीवन की समग्रता को नहीं पाया जा सकता। धर्म के द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान तो होता है, पर धर्म के द्वारा जीवन में पूर्ण तृप्ति का अनुभव नहीं होता। इतने वर्षों तक धर्म का पालन करते हुए भी मेरे जीवन में न तो भक्ति का उदय हुआ और न वैराग्य का। ये दो बड़े महत्त्व के सूत्र हैं। कर्म का परिणाम या तो भक्ति होना चाहिए या वैराग्य।
यदि जीवन में सुख-सुविधा प्राप्त हो तो इसका परिणाम तो यह हो सकता है कि हम यह विचार करें कि ये सब सुख सुविधाएँ जो हमें प्राप्त हुई हैं, ये ईश्वर की कृपा से मिली हैं। इससे भक्ति आ जायेगी। प्रभु के प्रति कृतज्ञता का उदय होगा। दुनिया में भी यदि किसी से आपको कुछ प्राप्त हो तो उसे धन्यवाद देते हैं और सोचते हैं कि हमें भी बदले में इनके पास कोई भेंट भेजनी चाहिए। हम कथा में सुन लेते हैं कि विपत्ति बहुत अच्छी होती है, विपत्ति में ही भगवान् कि भक्ति होती है, पर यह सत्य नहीं है। विपत्ति कोई याचना की वस्तु नहीं है, लेकिन यदि विपत्ति स्वयं आ जाय तो उसे भी हम प्रभु का भेजा हुआ प्रसाद मानकर स्वीकार करें। कुन्ती की विपत्ति याचना का प्रसंग पढ़कर हम उसका सही अर्थ समझें। कुन्ती भी अपने पुत्रों को विपत्ति में देखकर प्रसन्न नहीं होती थीं, दुःखी होती थीं। हाँ, जब भगवान् ने सब विपत्तियों का निवारण करके सम्पत्ति दे दी और तत्पश्चात् भगवान् विदा लेने लगे तब कुन्ती में अवसर विशेष की भावना हुई थी, वह जीवन भी सार्वजनीन भावना नहीं था।
कुन्ती से जब भगवान् विदा लेने लगे तो कुन्ती को लगा कि जो समप्ति भगवान् से विमुक्त कर दे उस समपत्ति से तो विपत्ति ही अच्छी है। यह शुस अवसर की विशेष प्रतिक्रिया थी, जिसका उद्देश्य भगवान् से यह प्रार्थना करना था कि आप कृपा करके मेरे समीप रहें। जो इस प्रसंग से प्रभावित होकर कुन्ती की माँग दोहराते रहते हैं, वे भी केवल शब्द मात्र दोहराते हैं। वस्तुतः वे भी विपत्ति नहीं माँगते। ‘रामायण’ में भी सुग्रीव एक ऐसा पात्र है। श्री हनुमानजी ने उनकी प्रभु से मित्रता करायी और प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि—
हम मूलतः ईश्वर के अंश होने से परम पवित्र हैं, परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि हम क्या बनने की चेष्टा कर रहे हैं ? दशरथ या दशमुख ? हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। दशरथ बनने की दिशा में कि दशमुख बनने की दिशा में। मनु बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने अपनी प्रजा को भी धर्मानुकूल चलाने की चेष्टा की, पर मनु को ऐसा लगा कि केवल धर्म के द्वारा जीवन की समग्रता को नहीं पाया जा सकता। धर्म के द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान तो होता है, पर धर्म के द्वारा जीवन में पूर्ण तृप्ति का अनुभव नहीं होता। इतने वर्षों तक धर्म का पालन करते हुए भी मेरे जीवन में न तो भक्ति का उदय हुआ और न वैराग्य का। ये दो बड़े महत्त्व के सूत्र हैं। कर्म का परिणाम या तो भक्ति होना चाहिए या वैराग्य।
यदि जीवन में सुख-सुविधा प्राप्त हो तो इसका परिणाम तो यह हो सकता है कि हम यह विचार करें कि ये सब सुख सुविधाएँ जो हमें प्राप्त हुई हैं, ये ईश्वर की कृपा से मिली हैं। इससे भक्ति आ जायेगी। प्रभु के प्रति कृतज्ञता का उदय होगा। दुनिया में भी यदि किसी से आपको कुछ प्राप्त हो तो उसे धन्यवाद देते हैं और सोचते हैं कि हमें भी बदले में इनके पास कोई भेंट भेजनी चाहिए। हम कथा में सुन लेते हैं कि विपत्ति बहुत अच्छी होती है, विपत्ति में ही भगवान् कि भक्ति होती है, पर यह सत्य नहीं है। विपत्ति कोई याचना की वस्तु नहीं है, लेकिन यदि विपत्ति स्वयं आ जाय तो उसे भी हम प्रभु का भेजा हुआ प्रसाद मानकर स्वीकार करें। कुन्ती की विपत्ति याचना का प्रसंग पढ़कर हम उसका सही अर्थ समझें। कुन्ती भी अपने पुत्रों को विपत्ति में देखकर प्रसन्न नहीं होती थीं, दुःखी होती थीं। हाँ, जब भगवान् ने सब विपत्तियों का निवारण करके सम्पत्ति दे दी और तत्पश्चात् भगवान् विदा लेने लगे तब कुन्ती में अवसर विशेष की भावना हुई थी, वह जीवन भी सार्वजनीन भावना नहीं था।
कुन्ती से जब भगवान् विदा लेने लगे तो कुन्ती को लगा कि जो समप्ति भगवान् से विमुक्त कर दे उस समपत्ति से तो विपत्ति ही अच्छी है। यह शुस अवसर की विशेष प्रतिक्रिया थी, जिसका उद्देश्य भगवान् से यह प्रार्थना करना था कि आप कृपा करके मेरे समीप रहें। जो इस प्रसंग से प्रभावित होकर कुन्ती की माँग दोहराते रहते हैं, वे भी केवल शब्द मात्र दोहराते हैं। वस्तुतः वे भी विपत्ति नहीं माँगते। ‘रामायण’ में भी सुग्रीव एक ऐसा पात्र है। श्री हनुमानजी ने उनकी प्रभु से मित्रता करायी और प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि—
सुन सुग्रीव मारिहउँ बालिहि एकहिं बान।4/6
सुनकर सुग्रीव के हृदय में क्षणिक वैराग्य का उदय हुआ। यह क्षणिक शब्द
बड़े महत्त्व का है। कुम्भकर्ण ने भी बड़ी उच्चकोटि की बातें कही थीं, पर
केवल उच्चकोटि का भाषण करना ही महत्ता का प्रमाण नहीं हो सकता। जब रावण ने
कुम्भकर्ण को जगाया तो कुम्भकर्ण ने रावण को फटकारा—
जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान।6/62
इतनी ही नहीं, यह भी लिखा हुआ है कि रावण को उपदेश देते-देते वह भगवान् का
ध्यान भी करने लगा, पर यह कुम्भकर्ण की श्रेष्ठता का द्योतक नहीं है। उस
पर व्यंग्य है—
राम रूप गुन सुमिरत मगन भयउ छन एक।
रावन मागेउ कोटि घट मद अरु महिष अनेक।।6/63
रावन मागेउ कोटि घट मद अरु महिष अनेक।।6/63
‘क्षण एक’ जो दो शब्द हैं, येही कुम्भकर्ण के चरित्र
के प्राण
हैं। ये शब्द सब कुछ कह गये। एक क्षण के लिए जब हम भगवान् के ध्यान में
डूब जाते हैं, ज्ञान, वैराग्य या भक्ति की बड़ी ऊँची-ऊँची बातें करने लग
जाते हैं तो उस क्षणिक ज्ञान, वैराग्य या भक्ति का कोई वास्तविक मूल्य है
क्या ? देखिए ! कुम्भकर्ण ने रावण को दुष्ट कहा और राम के ध्यान में डूब
गया तब तो रावण को निराश होना चाहिए था कि यह तो विभीषण की तरह राम का
भक्त हो गया, परन्तु तुरन्त ही रावण ने शराब के घड़े और भैंसे मँगवाये। यह
व्यंग्य है।
रावण कुम्भकर्ण को इतनी अच्छी तरह से पहचानता था कि उसे विश्वास था कि वह क्षणिक आवेश है, इसके बाद वह मदिरा पीकर मेरी ओर से ही लड़ेगा। विभीषण ने एक बार भी रावण का अपमान नहीं किया, कोई कठोर शब्द नहीं कहा, फिर भी रावण ने लात मारकर निकाल दिया और कुम्भकर्ण ने दुष्ट कह दिया, उपदेश भी दिया, उसके सामने ध्यान में भी बैठ गया, परन्तु फिर भी रावण मन-ही-मन हँसता है कि बच्चा ! हम तुम्हें जानते हैं कि तुम चाहे जितनी ऊँची-ऊँची बातें करो, पर तुम लड़ोगे हमारी ओर से ही। तुम भी अन्याय का ही पक्ष लोगे। क्षणिक आवेश ही दैत्य का चरित्र है। यही कुम्भकर्ण का और यही रावण का भी चरित्र है। सीताहरण के पूर्व सीताजी की फटकार सुनकर रावण भी मन में सीताजी को प्रणाम करता है—
रावण कुम्भकर्ण को इतनी अच्छी तरह से पहचानता था कि उसे विश्वास था कि वह क्षणिक आवेश है, इसके बाद वह मदिरा पीकर मेरी ओर से ही लड़ेगा। विभीषण ने एक बार भी रावण का अपमान नहीं किया, कोई कठोर शब्द नहीं कहा, फिर भी रावण ने लात मारकर निकाल दिया और कुम्भकर्ण ने दुष्ट कह दिया, उपदेश भी दिया, उसके सामने ध्यान में भी बैठ गया, परन्तु फिर भी रावण मन-ही-मन हँसता है कि बच्चा ! हम तुम्हें जानते हैं कि तुम चाहे जितनी ऊँची-ऊँची बातें करो, पर तुम लड़ोगे हमारी ओर से ही। तुम भी अन्याय का ही पक्ष लोगे। क्षणिक आवेश ही दैत्य का चरित्र है। यही कुम्भकर्ण का और यही रावण का भी चरित्र है। सीताहरण के पूर्व सीताजी की फटकार सुनकर रावण भी मन में सीताजी को प्रणाम करता है—
सुनत बचन दससीस रिसाना।
मन महुँ चरन बंदि सुख माना।।3/27/16
मन महुँ चरन बंदि सुख माना।।3/27/16
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book