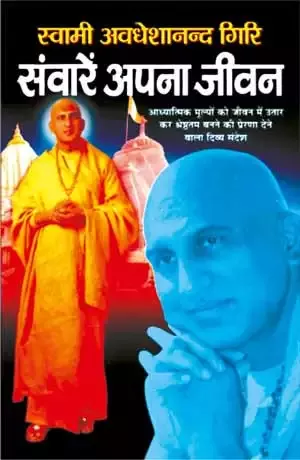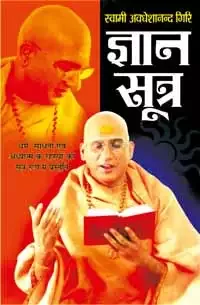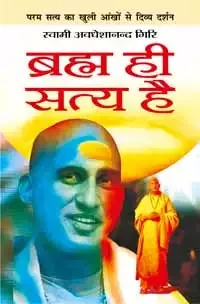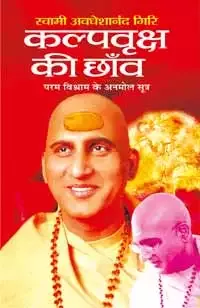|
धर्म एवं दर्शन >> संवारें अपना जीवन संवारें अपना जीवनस्वामी अवधेशानन्द गिरि
|
314 पाठक हैं |
||||||
श्रेष्ठ मनुष्य जीवन को श्रेष्ठतम बनाने वाला दिव्य संदेश
Sanvare Apna Jeevan
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
दो शब्द
जीवन न तो जन्म से शुरू होता है, और न ही मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने जन्म को अव्यक्त का व्यक्त होना और मृत्यु को व्यक्त का अव्यत्त होना कहा है। आत्मा अतींद्रिय है, इसलिए सामान्य संसारी व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, शरीर के अस्तित्व तक ही जीवन को मानता है।
सनातन वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार, जन्म-मृत्यु जीवन यात्रा के पड़ाव हैं। जीवनात्मा के जीवन में जन्म-मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है, जब तक वह अपनी आखिर मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। यह आखिरी पड़ाव ही आत्म साक्षात्कार है, इष्ट की प्राप्ति है। इस उपलब्धि के बाद सारी यात्रा समिट जाती है। इसके बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता।
धर्म ग्रन्थों में 84 लाख योनियों का वर्णन आता है। इनमें जाकर जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भोगती है। इसलिए इनकी संभावनाएं सीमित हैं। मनुष्य योनि का जो जगह-जगह गुणगान किया गया है, इसका कारण है इसका भोग योनि होने के साथ ही कर्मयोनि भी होना। इससे इसमें संभावनाएं भी अनंत हैं। इसी अर्थ में यह सुरदुर्लभ है। देवयोनि यद्यपि मनुष्य योनि से श्रेष्ठ है लेकिन उसमें सदैव अधःपतन का भय रहता है उसका अतिक्रमण करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता है, इसलिए धर्मशास्त्रों की रचना मनुष्य के लिए की गई। सारे विधि-निषेध नियम मनुष्य के लिए बनाए गए-न तो ये पशु-पक्षियों आदि के लिए हैं, न ही देवताओं के लिए।
मनुष्य जीवन की सार्थकता विषय भोगों में लिप्त रहना नहीं है, क्योंकि इस संदर्भ में अन्य योनियों की अपेक्षा मनुष्य अत्यंत निर्बल है। चाहें तो अलग-अलग तुलना करके देख सकते हैं।
धर्मशास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की चर्चा की गई है। पहले तीन को उन्होंने पुरुषार्थ कहा है जबकि मोक्ष को पर पुरुषार्थ। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम ये तीन उपलब्धियां हैं मनुष्य जीवन की। जबकि मोक्ष परम उपलब्धि है। धर्मशास्त्र इस विवेचन द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि यदि ‘मोक्ष’ की उपलब्धि नहीं हुई, तो तीनों की कोई सार्थकता नहीं है।
महामंडलेश्वर जूनापीठाधीश्वर श्री स्वामी अवधेशानन्द जी महाराज के प्रवचनों में इसी यथार्थ को तरह-तरह से समझने का आपको सुअवसर प्राप्त होता है। स्वामीजी द्वारा कहा गया एक-एक शब्द समूचे व्यक्तित्व को गहराई तक छूता है। महाराजश्री की प्रांजल भाषा का संपूर्ण रूप से स्पर्श करना दुष्कर कार्य है। लेकिन फिर भी मैंने जनहित के लिए उन्हीं की परम कृपा से उसे शब्दों में बांधने की, सुगमरूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। महाराजश्री के अनुसार, शरीर को सजाना-संवारना व्यावहारिक दृष्टि से यह मात्र आत्म प्रवंचना है—स्वयं को धोखा देना है। अपने जीवन में शरीर के बदलाव संकेत देते हैं कि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व (चरित्र) को संवारना चाहिए।
इसी से लोक-परलोक संवरते हैं। आत्मिक विकास ही सच्चे अर्थों में स्वयं को संवारना है।
स्वामी जी ने श्रवण के साथ मनन, निदिध्यासन पर भी जोर दिया है। उनका परामर्श है कि श्रेय मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जिस तरह संकल्प की आवश्यकता होती, उसे सिर्फ सत्संग, स्वाध्याय, सेवा और ईश्वर चिंतन से ही प्राप्त किया जा सकता है।
आप सबके जीवन में श्रेय का मार्ग प्रशस्त हो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं।
सनातन वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार, जन्म-मृत्यु जीवन यात्रा के पड़ाव हैं। जीवनात्मा के जीवन में जन्म-मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है, जब तक वह अपनी आखिर मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। यह आखिरी पड़ाव ही आत्म साक्षात्कार है, इष्ट की प्राप्ति है। इस उपलब्धि के बाद सारी यात्रा समिट जाती है। इसके बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता।
धर्म ग्रन्थों में 84 लाख योनियों का वर्णन आता है। इनमें जाकर जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भोगती है। इसलिए इनकी संभावनाएं सीमित हैं। मनुष्य योनि का जो जगह-जगह गुणगान किया गया है, इसका कारण है इसका भोग योनि होने के साथ ही कर्मयोनि भी होना। इससे इसमें संभावनाएं भी अनंत हैं। इसी अर्थ में यह सुरदुर्लभ है। देवयोनि यद्यपि मनुष्य योनि से श्रेष्ठ है लेकिन उसमें सदैव अधःपतन का भय रहता है उसका अतिक्रमण करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता है, इसलिए धर्मशास्त्रों की रचना मनुष्य के लिए की गई। सारे विधि-निषेध नियम मनुष्य के लिए बनाए गए-न तो ये पशु-पक्षियों आदि के लिए हैं, न ही देवताओं के लिए।
मनुष्य जीवन की सार्थकता विषय भोगों में लिप्त रहना नहीं है, क्योंकि इस संदर्भ में अन्य योनियों की अपेक्षा मनुष्य अत्यंत निर्बल है। चाहें तो अलग-अलग तुलना करके देख सकते हैं।
धर्मशास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की चर्चा की गई है। पहले तीन को उन्होंने पुरुषार्थ कहा है जबकि मोक्ष को पर पुरुषार्थ। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम ये तीन उपलब्धियां हैं मनुष्य जीवन की। जबकि मोक्ष परम उपलब्धि है। धर्मशास्त्र इस विवेचन द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि यदि ‘मोक्ष’ की उपलब्धि नहीं हुई, तो तीनों की कोई सार्थकता नहीं है।
महामंडलेश्वर जूनापीठाधीश्वर श्री स्वामी अवधेशानन्द जी महाराज के प्रवचनों में इसी यथार्थ को तरह-तरह से समझने का आपको सुअवसर प्राप्त होता है। स्वामीजी द्वारा कहा गया एक-एक शब्द समूचे व्यक्तित्व को गहराई तक छूता है। महाराजश्री की प्रांजल भाषा का संपूर्ण रूप से स्पर्श करना दुष्कर कार्य है। लेकिन फिर भी मैंने जनहित के लिए उन्हीं की परम कृपा से उसे शब्दों में बांधने की, सुगमरूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। महाराजश्री के अनुसार, शरीर को सजाना-संवारना व्यावहारिक दृष्टि से यह मात्र आत्म प्रवंचना है—स्वयं को धोखा देना है। अपने जीवन में शरीर के बदलाव संकेत देते हैं कि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व (चरित्र) को संवारना चाहिए।
इसी से लोक-परलोक संवरते हैं। आत्मिक विकास ही सच्चे अर्थों में स्वयं को संवारना है।
स्वामी जी ने श्रवण के साथ मनन, निदिध्यासन पर भी जोर दिया है। उनका परामर्श है कि श्रेय मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जिस तरह संकल्प की आवश्यकता होती, उसे सिर्फ सत्संग, स्वाध्याय, सेवा और ईश्वर चिंतन से ही प्राप्त किया जा सकता है।
आप सबके जीवन में श्रेय का मार्ग प्रशस्त हो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं।
गंगा प्रसाद शर्मा
मैं बिलकुल निर्दोष हूं,
कहां हैं मुझमें दोष ?
मैं भूल करता आ रहा हूं न जाने कब से
स्वयं को दोषी समझने की
प्रकृति के गुण-दोषों को मैंने अपना माना
जो झूठ था—सफेद झूठ, उसे मैंने सच माना
लेकिन अब...
अब नोच डाला है मैंने तन-मन के दोषों को
संवार लिया है मैंने खुद को
और बन गया हूं स्वयं खुदा
जिसका स्पर्श तक नहीं कर सकते दोष
अब नहीं रहा है शेष कुछ भी पाना
मैं निर्दोष हूं
‘सोऽहम्’
वेदांत तीर्थ
1
संत समागम
हिन्दी साहित्य में ‘संत’ शब्द को ‘सत्य’ या ‘सत्’ का पर्यायवाची माना जाता है जो सात्विक, उदार, मोह-माया एवं छल-प्रपंच से दूर तथा ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करने वाला होता है। लेकिन वैदिक साहित्य में ‘संत्’ को ‘परमात्मा’ या ‘ब्रह्मा’ का रूप कहा जाता है। इसी प्रकार का अर्थ पौराणिक साहित्य में भी मिलता है। ‘छांदोग्य उपनिषद्’ और ‘ऋग्वेद’ में कहा गया है कि संत अर्थात् ज्ञानीजन उस अद्वितीय पुरुष की अनेक रूपों में स्तुति करते हैं जो परब्रह्म है। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास ने ‘रामायण’ (उत्तरकांड) में इसी भाव से प्रेरित होकर संत और अनंत को एक समान माना है। यथा—जानेसु संत अनंत समाना।
‘संत’ शब्द ‘संति’ एवं ‘सत्य’ शब्द का अपभ्रंश है जो हिन्दी में एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन यह संस्कृत भाषा के ‘अस’ धातु और ‘शतृ’ प्रत्यय से बना पुल्लिंग शब्द है। संत शब्द की सामान्य परिभाषा है—जो सबक् कल्याण करे, उसे संत कहते हैं। परंतु ‘अस’ धातु और ‘शतृ’ प्रत्यय से बने शब्द का अर्थ है—जो हो सकता है अर्थात् अस्तित्व। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किसी ऐसी वस्तु या पद के लिए होता है जो सदा नित्य, निर्विकार, एक समान और विकारहीन रूप में विद्यामान हो।
आदि शंकराचार्य ने संत शब्द की परिभाषा करते हुए कहा है अखिलवीतरागाः अपास्मोहःशिवतत्वनिष्ठः अर्थात् जिसका विषयों में राग समाप्त हो चुका है, जो भली भांति जान चुका है, कि विषयों की प्राप्ति से सुख का कोई संबंध नहीं है, जो सदैव है जिसे किसी भी प्रकार की कोई मूर्च्छा नहीं है, जो सत्य-असत्य को स्पष्ट देख रहा है, जिसकी शिवतत्व और परमतत्व में पूर्ण निष्ठा है और जो सदैव कल्याण में स्थित है; वही संत है। इस परिभाषा द्वारा आदि शंकराचार्य ने इन्द्रियजन्य सुख, मानसिक धरातल के सुख-दुख, सही-गलत जैसी मान्यताओं और आध्यात्मिक स्तर पर अस्तित्व की स्वीकृति आदि संपूर्ण व्यक्तित्व का संस्पर्श किया है। इस प्रकार संत का अर्थ है जो परमार्थ में सतत अनायास रूप से तत्पर हो।
अंग्रेजी भाषा का सेंट (Saint) शब्द वस्तुतः लैटिन से सैंक्टस (Sanctus) शब्द से बना है जिसका अर्थ है—पवित्र। यह शब्द ईसाई धर्म के कुछ अत्यंत प्राचीन महात्माओं के लिए पवित्रात्मा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हिंदी में प्रचलित शब्द ‘संत’ एवं ‘साईं’ एक समान हैं। संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत् रूपी परमतत्व का अनुभव करके अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ उसी के समान हो गया है। दूसरों शब्दों में, जो सत्य स्वरूप नित्य का साक्षात्कार कर चुका है अथवा अपनी साधना के फलस्वरूप उसी अखंड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है, वही संत है।
इस प्रकार संतों में अति मानवीय गुणों का समावेश अवश्य होता है।
यह गुण हवा में उड़ने या पानी में चलने के समान नहीं होता जैसा कि लोगों को भ्रम होता है। उनमें दया, दान, क्षमा, परोपकार, सेवा-सद्भाव, अभेद, निवैरता तथा शांत चित्त आदि गुण होते हैं जो सामान्य मनुष्यों में नहीं पाए जाते। इन गुणों के अभाव के कारण ही मनुष्य साधारण बना रहता है। वह अपने स्तर से ऊपर नहीं उठ पाता। लेकिन जो साधक मनुष्य भावात्मक परिस्थितियों में अविचलित, प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ और अपनी संकल्प-शक्ति भाव-शक्ति के बीच उचित सामंजस्य बनाए रखकर सभी प्राणियों में ईश्वर का रूप देखता है, वही संत कहलाता है। ‘श्रीमद्भागवद् गीता’ में इस अवस्था को भी ‘सत्’ कहा गया है जिसमें कोई मनुष्य यज्ञ, तप और दान में स्थिर बुद्धि रखता है।
संत के लक्षण बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं—संत वह है जो अपनी भावनाओं और वासनाओं से ऊपर उठकर उन सभी स्थितियों में अविचल रहे जिनमें साधारण मनुष्य का मन चंचल हो सकता है। इसके अलावा सभी लोगों को सदा समान समझता हुआ निरंतर उनके कल्याण में निरत रहे। इस प्रकार योगी, संत अथवा त्यागी में भारी अंतर है।
‘संत’ शब्द ‘संति’ एवं ‘सत्य’ शब्द का अपभ्रंश है जो हिन्दी में एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन यह संस्कृत भाषा के ‘अस’ धातु और ‘शतृ’ प्रत्यय से बना पुल्लिंग शब्द है। संत शब्द की सामान्य परिभाषा है—जो सबक् कल्याण करे, उसे संत कहते हैं। परंतु ‘अस’ धातु और ‘शतृ’ प्रत्यय से बने शब्द का अर्थ है—जो हो सकता है अर्थात् अस्तित्व। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किसी ऐसी वस्तु या पद के लिए होता है जो सदा नित्य, निर्विकार, एक समान और विकारहीन रूप में विद्यामान हो।
आदि शंकराचार्य ने संत शब्द की परिभाषा करते हुए कहा है अखिलवीतरागाः अपास्मोहःशिवतत्वनिष्ठः अर्थात् जिसका विषयों में राग समाप्त हो चुका है, जो भली भांति जान चुका है, कि विषयों की प्राप्ति से सुख का कोई संबंध नहीं है, जो सदैव है जिसे किसी भी प्रकार की कोई मूर्च्छा नहीं है, जो सत्य-असत्य को स्पष्ट देख रहा है, जिसकी शिवतत्व और परमतत्व में पूर्ण निष्ठा है और जो सदैव कल्याण में स्थित है; वही संत है। इस परिभाषा द्वारा आदि शंकराचार्य ने इन्द्रियजन्य सुख, मानसिक धरातल के सुख-दुख, सही-गलत जैसी मान्यताओं और आध्यात्मिक स्तर पर अस्तित्व की स्वीकृति आदि संपूर्ण व्यक्तित्व का संस्पर्श किया है। इस प्रकार संत का अर्थ है जो परमार्थ में सतत अनायास रूप से तत्पर हो।
अंग्रेजी भाषा का सेंट (Saint) शब्द वस्तुतः लैटिन से सैंक्टस (Sanctus) शब्द से बना है जिसका अर्थ है—पवित्र। यह शब्द ईसाई धर्म के कुछ अत्यंत प्राचीन महात्माओं के लिए पवित्रात्मा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हिंदी में प्रचलित शब्द ‘संत’ एवं ‘साईं’ एक समान हैं। संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत् रूपी परमतत्व का अनुभव करके अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ उसी के समान हो गया है। दूसरों शब्दों में, जो सत्य स्वरूप नित्य का साक्षात्कार कर चुका है अथवा अपनी साधना के फलस्वरूप उसी अखंड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है, वही संत है।
इस प्रकार संतों में अति मानवीय गुणों का समावेश अवश्य होता है।
यह गुण हवा में उड़ने या पानी में चलने के समान नहीं होता जैसा कि लोगों को भ्रम होता है। उनमें दया, दान, क्षमा, परोपकार, सेवा-सद्भाव, अभेद, निवैरता तथा शांत चित्त आदि गुण होते हैं जो सामान्य मनुष्यों में नहीं पाए जाते। इन गुणों के अभाव के कारण ही मनुष्य साधारण बना रहता है। वह अपने स्तर से ऊपर नहीं उठ पाता। लेकिन जो साधक मनुष्य भावात्मक परिस्थितियों में अविचलित, प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ और अपनी संकल्प-शक्ति भाव-शक्ति के बीच उचित सामंजस्य बनाए रखकर सभी प्राणियों में ईश्वर का रूप देखता है, वही संत कहलाता है। ‘श्रीमद्भागवद् गीता’ में इस अवस्था को भी ‘सत्’ कहा गया है जिसमें कोई मनुष्य यज्ञ, तप और दान में स्थिर बुद्धि रखता है।
संत के लक्षण बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं—संत वह है जो अपनी भावनाओं और वासनाओं से ऊपर उठकर उन सभी स्थितियों में अविचल रहे जिनमें साधारण मनुष्य का मन चंचल हो सकता है। इसके अलावा सभी लोगों को सदा समान समझता हुआ निरंतर उनके कल्याण में निरत रहे। इस प्रकार योगी, संत अथवा त्यागी में भारी अंतर है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book