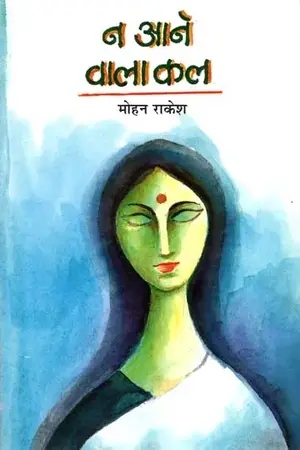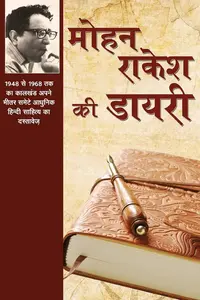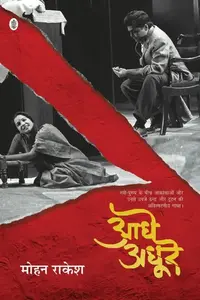|
उपन्यास >> न आने वाला कल न आने वाला कलमोहन राकेश
|
361 पाठक हैं |
|||||||
"बदलते समय की छाया में जीवन के क्षणों की झलक।"
लेकिन क्या निश्चय ?
मैं उन सब विकल्पों पर विचार करने लगा जिनके सहारे अपने को इससे आगे सोचने से रोका जा सकता था।
विकल्प एक-उठकर कपड़े बदले जाएँ। खाना बाहर किसी होटल में खाया जाए। फिर रात को शो देखकर सोने के समय घर लौटा जाए-अर्थात् जब बीच का पूरा अन्तराल तय हो चुका हो।
विकल्प दो-ड्रेसिंग गाउन पहनकर एन.के.के. यहां चला जाए। दो घंटे उससे उसकी प्रेमिका अर्थात् होने वाली पत्नी के पत्र सुने जाएँ। फिर सुबह तक उसके उस खाली बिस्तर में दुबक रहा जाए जो उसने अभी से फरवरी में होने वाली अपनी शादी की प्रतीक्षा में बिछा रखा है।
विकल्प तीन-जेबों में हाथ डाले लोअर माल का एक चक्कर लगा लिया जाय। एकाध डब्बी सिगरेट खरीदकर फूंक डाली जाए। फिर इस तरह घर की तरफ लौटा जाए जैसे उतनी देर बाहर रहकर किसी से किसी चीज़ का कुछ तो बदला ले ही लिया हो।
विकल्प चार...
मैं सोया-चेयर से उठ खड़ा हुआ। इनमें से कुछ भी करने में कोई तुक नहीं था क्योंकि सब बातें पहले की आजमाई हुई थीं। कमरे में जाकर मैंने स्कूल से आया टिफिन कैरियर खोल लिया। खाना गरम करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए दो बोटी ठण्डा गोश्त सूप के साथ निगल लिया। फिर टिफिन के जूठे डब्बों को इस तरह गुसलखाने में पटक दिया जैसे कि खाने के बदमज़ा होने की सारी ज़िम्मेदारी उन्हीं पर हो।
‘मुझे पता है, मैं क्या चाहता हूँ,’ गुसलखाने का दरवाज़ा बन्द करते हुए मैंने सोचा फिर उसे करने में मुझे इतनी रुकावट क्यों महसूस हो रही है ?’
खट् खट् खट् साथ के पोर्शन से आती आवाज़ ने कुछ देर के लिए ध्यान बँटा दिया। कोहली की बीवी शारदा खड़ाऊँ पहने अपने गुसलखाने की तरह जा रही थी। शाम के सात बजे से लेकर रात के दो बजे तक वह जाने कितनी बार गुसलखाने में जाती थी। कभी गुरदे साफ करने के लिए, कभी प्लेटें धोने के लिए और कभी अन्दर बन्द होकर रोने के लिए। बीच में पक्की दीवार होने के बावजूद उसकी खड़ाऊँ से मेरे पोर्शन का फर्श भी हिल जाता था। आधी पात को तो लकड़ी के फर्श पर वह खट् खट् की आवाज़ बहुत ही मनहूस लगती थी।
मैं बरामदे में आकर अपनी पढ़ने की मेज़ के पास बैठ गया। चिट्ठी लिखने का कागज़ निकालकर सामने रख लिया। कलम खोल लिया। फिर भी तब तक अपने को लिखने से रोके रहा जब तक शारदा के पैरों की खट्-खट् गुसलखाने से वापस नहीं आ गई। उसके बाद लिखना शुरू किया-‘प्रिय शोभा....’
मन में यह पत्र मैं कई बार लिख चुका था। लिखकर हर बार मन में ही उसे फाड़ दिया था। उस समय वे दो शब्द कागज़ पर लिख लेना मुझे काफी हिम्मत का काम लगा। मैं कुछ देर चुपचाप उन्हें देखता रहा। कैमल रंग के दानेदार कागज़ पर वे दोनों शब्द ‘प्रिय’ और ‘शोभा’ सतह से ऊपर को उठे-से लग रहे थे। दोनों अलग-अलग। बल्कि सभी अक्षर अलग-अलग प्रि य शो भा। मैंने उन अक्षरों पर लकीर फेर दी और कागज को मसलकर टोकरी में फेंक दिया। एक कोरा कागज़ लेकर फिर से लिखना शुरू किया शोभा।
रुककर जेबें टटोली। डब्बी में एक ही सिगरेट था। सोचा कि अगर घूमने निकल गया होता, तो कुछ सिगरेट तो और खरीद ही लाता। छः आठ सिगरेट पास में होते तो पत्र आसानी से पूरा किया जा सकता था।
मैंने सिगरेट सुलगा लिया। बस पहली पंक्ति लिखना ही मुश्किल था। उसके बाद बाकी मजमून के लिए रुकने की सम्भावना नहीं थी।
सामने के स्याह काँच को देखते हुए मैंने एक लम्बा कश खींचा शोभा पास में होती, तो उस तरह कश खींचने से मुझे रोकती तो नहीं, पर एक शहीदाना भाव आँखों में लाकर चुपचाप मुझे देखती रहती। उसकी आँखों के उस शहीदाना भाव को सहना ही मुझे सबसे मुश्किल लगता था। लगता कि वह मुझे देख नहीं रही, मन-ही-मन उस दूसरे के साथ मेरी तुलना कर रही है जिसके साथ विवाहित जीवन के सात साल उसने पहले बिताए थे। हालाँकि उस दूसरे का नाम वह जबान पर नहीं लाती थी-अपने सारे व्यवहार से यही प्रकट करने का प्रयत्न करती थी कि यह उसकी पहली शादी है-फिर भी अपने मन से वह जीती उस खोई हुई जिन्दगी में ही थी। इसीलिए उसकी आँखों में वह शहीदाना भाव दिन में कई-कई बार नज़र आ जाता था। सुबह उठने से रात को सोने तक वह बात-बात पर शहीद होती थी। मेरा हँसना, बात करना, खीझना कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे शहीद होने के लिए मजबूर न करता हो, बातचीत के दौरान मेरे मुँह से कभी उसके पहले पति का नाम निकल जाता, तो उसे लगता जैसे जान-बूझकर उसे छीलने की कोशिश की गई हो।
और उसकी शहीद होते रहने की आदत के कारण मैं भी अपने को शहीद होने के लिए मजबूर पाता था। उसके जूड़े से बाहर निकली पिंनें, साड़ी से नीचे को झाँकता पेटीकोट, आँखों में लदा-लदा सुरमा और फड़कती नसें लिए बात के बीच से उठ जाने का ढंग-बहुत कुछ ऐसा था जिसके लिए मैं उसे टोकना चाहता था, पर टोक नहीं पाता था। कुछ दिनों के परिचय की झोंक में शादी तो मैंने उससे कर ली थी, पर अब लगता था कि अन्दर के एक डर से अपने को कमजोर पाकर ही मैंने ऐसा किया था। शादी से पहले एक बार मैंने उससे कहा भी था कि पैंतीस की उम्र तक अकेला रहकर मैं अपने को बहुत थका हुआ महसूस करने लगा हूँ। तब उसने बहुत समझदारी के साथ आँखें हिलाई थीं-जैसे कि यह कहकर मैंने अपनी तब तक की ज़िन्दगी के लिए पश्चाताप प्रकट किया हो। मुझे पहली बार मिलने पर ही लगा था’, उसने कहा था, ‘आदमी अपने मनबहलाव के लिए चाहे जितने उपाय कर ले, पर रात-दिन का अकेलापन उसे तोड़कर रख देता है।’ इस बात में उसका हल्का-सा संकेत अपने पिता से सुनी बातों की तरफ भी था। मैंने उस संकेत को नहीं उठाया था क्योंकि खामखाह की लम्बी व्याख्या में मैं नहीं पड़ना चाहता था।
उसने मेरे घर में आकर एक नई शुरूआत की कोशिश की थी, पर वह शुरुआत सिर्फ उसके अपने लिए थी। उस शुरुआत में मुझे उसके लिए वही होना चाहिए था जो कि वह दूसरा था जिसकी वह सात साल आदी रही थी। घर कैसे होना चाहिए, खाना कैसा बनना चाहिए, दोस्ती कैसे लोगों से रखनी चाहिए-इस सबके उसके बने हुए मानदण्ड थे जिनसे अलग हटकर कुछ भी करना उसे बुनियादी तौर पर गलत जान पड़ता था। शुरू में जब मैं अपने ढंग से कुछ भी करने की जिद करता, तो वह आँखों में रुआंसा भाव लाकर पलकें झपकाती हुई सिर्फ एक ही शब्द कहती, ‘अरे !’ मैं उस ‘अरे !’ की चुभन महसूस करता हुआ एक उसांस भरकर चुप रह जाता, या मन में कुढ़ता हुआ कुछ देर के लिए घर से चला जाता। तब लौटकर आने पर वह रोए चेहरे से घर के काम करती मिलती। उसकी नज़र में मैं अब भी एक अकेला आदमी था जिसका घर उसे संभालना पड़ रहा था जबकि मेरे लिए वह किसी दूसरे की पत्नी थी जिसके घर में मैं एक बेतुके मेहमान की तरह टिका था। मैं कोशिश करता था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर से बाहर रह सकूँ, रहूँ। पर जब मजबूरन घर में रुकना पड़ जाता, तो वह काफी देर के लिए साथ के पोर्शन में शारदा के पास चली जाती थी।
बीच में एक बार उसे कॉलिक का दौरा पड़ा था। तब कर्नल बत्रा ने जो दवाइयाँ लिखकर दीं, वे उसने मुझे नहीं लाने दीं। कागज़ पर कुछ और दवाइयों के नाम लिख दिए तो कुछ साल पहले वैसा ही दौरा पड़ने पर उसे दी गई थीं। मैंने उससे कहा भी कि जिस डॉक्टर को दिखाया है, उसी की दवाई उसे लेनी चाहिए। पर वह अपने हठ पर अड़ी रही ‘‘मुझे अपने जिस्म का पता है,’’ उसने कहा। ‘‘मुझे आराम आएगा, तो उन्हीं दवाइयों से जो मैं पहले ले चुकी हूँ। जब मैं कहती हूँ कि मुझे वही दवाइयाँ चाहिए, तो तुम इन दवाइयों के लिए हठ क्यों करते हो ?’’
मैंने हठ नहीं किया। वह अपनी दवाइयों से तीन-चार दिन में ठीक भी हो गई। उसे सचमुच अपनी दवाइयों का पता था, खान-पान के परहेज़ का पता था। और भी प्रायः सभी चीज़ों का पता था-उन किताबों का जो उसे पढ़नी चाहिए थीं, उन जगहों का जहाँ उसे जाना चाहिए था और उसे सारे तौर-तरीके का जिससे एक घर में अच्छी ज़िन्दगी जी जा सकती थी। अगर कुछ सीखने को था, तो सिर्फ मेरे लिए था क्योंकि इतने साल अकेली ज़िन्दगी जीने के कारण मुझे किसी भी सही चीज़ का बिलकुल पता नहीं था’ साथ रहने के कुछ महीनों में हमें एक-दूसरे की इतनी आदत तो हो ही गई थी कि हमने एक-दूसरे के मामले में दखल देना छोड़ दिया था। मुझे मन में जितना गुस्सा आता था, बाहर मैं उतने ही कोमल ढंग से बात करता था। वह भी ऐसा ही करती थी। एक-दूसरे की बढ़ती पहचान हमारे अन्दर एक औपचारिकता में ढलती गई थी। यह जान लेने के बाद कि न तो हम अपनी-अपनी हदें तोड़ सकते हैं और न ही एक-दूसरे ही हदबन्दी को पार कर सकते हैं, हमने एक युद्ध विराम में जाना शुरू कर दिया था। उस युद्ध विराम की दोनों की अपनी-अपनी शर्तें थीं-अपने-अपने तक सीमित। दोनों को एक-दूसरे से कुछ आशा नहीं थी, इसलिए हदबन्दी टूटने की नौबत बहुत कम आती थी।
|
|||||