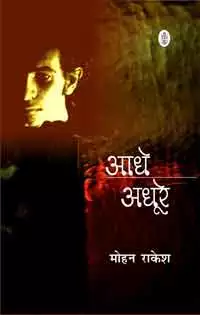|
उपन्यास >> न आने वाला कल न आने वाला कलमोहन राकेश
|
361 पाठक हैं |
||||||
तेजी से बदलते जीवन तथा व्यक्ति तथा उनकी प्रतिक्रियाओं पर आधारित उपन्यास...
चेपल में जो कुछ हुआ, वह नया नहीं था। कुछ साम गाए गए। पादरी ने प्रार्थनाएँ कीं। घुटनों के बल होकर आँखों पर हाथ रखे लोगों ने प्रार्थनाओं को दोहरा दिया। अन्त में पादरी बेन्सन ने सैंतीत मिनट का सर्नम दिया। स्कूल-मास्टर होने के नाते उसका सर्मन पूरे एक पीरियड का होता था...चालीस में से हाज़िरी के तीन मिनट निकालकर। मैं बगलों में हाथ दबाए उतनी देर चेपल की दीवारों और लोगों के हिलते सिरों को देखता रहा। लगातार सैंतीस मिनट बिना किसी प्रतिकिया के, एक ही आदमी की आवाज़ सुनते जाना काफी धीरज का काम था-खास तौर से एक गैर ईसाई के लिए। पर मुझे इसकी आदत हो चुकी थी। अपनी सारी स्थिरता कूल्हों और टाँगों तक सीमित किए ऊपर से बुत-सा बना बैठा रहता था। अपने को व्यक्त रखने के लिए बिना घड़ी की तरफ देखे समय का अनुमान लगाता और उसे घड़ी से मिलाकर देखता रहता था। उसी तह जैसे में सफर करते हुए एक आदमी तय किए फासले का अपना अनुमान मील के पत्थरों से मिलाकर देखता है। जितनी बार अनुमान सही निकलता, मुझे अपने में एक इण्टयूशन का अहसास होता। इण्टयूशन की वैज्ञानिकता में विश्वास, होने लगता। पर जितनी बार अनुमान गलत निकल आता, उतनी बार मन इस विषय में नास्तिक होने लगता। चेपल से उठते समय मेरी आस्तिकता या नास्तिकता इस पर निर्भर करती थी कि अन्तिम बार का मेरा अनुमान सही निकला था या गलत। पर कई बार वह कुछ दूसरे कारणों पर भी निर्भर करती थी।
चेपल के अन्दर उस पर काफी ठण्ड थी-वह खास ठण्ड जो कि एक चेपल के अन्दर ही होती है। उस ठण्ड से, अन्दर की रोशनी के बावजूद, बाहर गहरा सांझ का कुछ-कुछ आभास मिल रहा था। हालाँकि मेरे खून की तपिश उस समय भी कम नहीं थी, फिर भी मेरे हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे थे। ठण्ड का असर नाक और माथे पर भी हो गया था, जिससे डर लग रहा था कि कहीं सर्मन के दौरान ही न छींकने लगूँ। रूमाल पास में नहीं था, यह मैं जेबों में टटोलकर देख चुका था। त्रिशूली में एक जगह हम लोग अपने-अपने रूमाल बिछाकर बैठे थे।
शायद वहीं भूल आया था। ऐसे में हालत यह थी कि अपने पर वश रखने के लिए मुझे बार-बार थूक निगलना पड़ रहा था। आँखों और कानों से मैं यह अनुमान लगाने की भी कोशिश कर रहा था कि उस हालत में वहाँ अकेला मैं ही हूँ या कोई और भी मेरी तरह उस यन्त्रणा में से गुजर रहा है। मेरा ख्याल है मिसेज दारुवाला की स्थिति भी वैसी ही थी। वह जैसे सर्मन से अभिभूत होकर बार-बार अपनी आँखों को रूमाल से छू रही थी। पर रूमाल आँखों के अलावा उसकी नाक और होंठों को भी ढक लेता, इससे वास्तविकता कुछ और ही जान पड़ती थी। मेरी नास्तिकता उस समय काफी बढ़ गई थी, क्योंकि मेरा समय का अनुमान तीन बार गलत निकल चुका था। आखिर सर्मन समाप्त हुआ। बाहर निकलने से पहले आखिरी प्रार्थना की जाने लगी। अपने को छींकने से रोके रहने के कारण मेरी हालत उस बच्चे की-सी हो रही थी जो कमोड की तरह भागना चाहते हुए भी बड़ों के डर से अच्छा बच्चा बना बैठा हो। पर चेपल से बाहर आते ही और जरा देर अच्छा बच्चा बने रहना मुझे सम्भव नहीं लगा। इसलिए ‘गुड नाइट मिस्टर सो एण्ड सो’, और गुड नाइट मिसेज़ सो एण्ड सो का रुटीन पूरी करना के लिए मैं कारिडोर में नहीं रुका। इसके पहेल कि मिस्टर और मिसेज़ व्हिलसर चेपल से बाहर आएँ, पीछे का रास्ता पकड़कर सड़क पर निकल आया। घर पहुँचकर अलमारी से दूसरा रूमाल निकालने तक मेरा छींक-छींककर बुरा हाल हो गया।
गरम पानी के साथ थोड़ी-सी ब्रांडी लेकर दस मिनट में मैंने अपने को ठीक कर लिया। अब मैं था और वह खालीपन जिसके साथ रोज रात को बारह बजे तक संघर्ष करना होता था। अगर हफ्ते के बीच का कोई दिन होता, तो दो घण्टे के लिए माल पर निकल जाता। घर से लोअर माल और लोअर माल से माल की चढ़ाई चढ़ने में ही एक निरर्थक-सी सार्थकता का अनुभव कर लेता। पर माल पर जाकर जिन लोगों से मिलना होता था, उनसे पहले ही दिन भर ऊबकर आया था। यूँ भी उनसे मिलना मिलने के लिए न होकर किसी चीज़ के एवज़ में होता था और एवज़ की वे आकृतियाँ तब तक भी शायद त्रिशूली से अपर रिज के रास्ते में किसी पेड़ के नीचे लुढ़क रही थीं। अभी सात नहीं बजे थे। सोने से पहले के पाँच छः घंटे ऐसे थे कि उनकी हदबन्दी किसी के सर्मन से नहीं होती थी। वह सिर्फ खाली समय था-खाली समय-जिसे बिना किसी विराम चिन्ह के एक-एक मिनट करके आगे बढ़ना था। उस बीच काम सिर्फ एक ही था-बिना भूख के खाना खाना-जिसे समय के उस पूरे फैलाव में अपनी मर्ज़ी से इधर या उधर को सरकाया जा सकता था।
‘अब ? मैंने आईने में अपना चेहरा देखा। पचीस वाट की रोशनी में वह काफी बेजान-सा लगा। कुछ-कुछ डरावना भी। जैसे कि उसके उभार अलग हों, गहराइयाँ अलग। मैंने आईने के पास से हटते हुए दोनों हाथों से चेहरे को मल लिया। ‘अब ?’
कुछ था जो किया जाना था। लेकिन क्या ?
मैंने कमरे में खड़े होकर आसपास के सामान को देखा। दो कबर्ड, दो पलंग। एक चेस्ट आफ् ड्राअर्ज। एक ड्रेसिंग टेबल। दो कुर्सियाँ। एक तिपाई। सब कुछ उस ज़माने का जिस ज़माने में वह कोठी बनी थी, या जिस ज़माने स्कूल बना था। तब से अब तक का सारी घिसाई के बावजूद अपनी ज़गह मज़बूत। बाहर बरामदे में एक पहियेदार सोफा और दो सोफा चेयर। तीनों के स्प्रिंग अलग-अलग तरफ को करवट लिए। बीस साल पहले के परदे; न जाने किस रंग के। उतने ही साल पहले की दरी। शराब, शोरबा, स्याही और बच्चों की हाजत कें निशान लिए। सब कुछ बीता हुआ, जिया जा चुका है, फिर भी जहाँ का तहाँ। मुझसे पहले जाने किस-किसका, पर आज मेरा। मेरा अर्थात् स्कूल के हिन्दी मास्टर का। तीन साल पहले तक हिन्दी मास्टर का नाम था नरुला। आज नाम था सक्सेना। मनोज सक्सेना अर्थात् शिवचन्द्र नरूला अर्थात् वह अर्थात् मैं अर्थात हम दोनों में से कोई नहीं अर्थात् हिन्दी-मास्टर फादर बर्टन स्कूल। मैं कमरे से बरामदे में आ गया और जिस सोफा चेयर के स्प्रिंग जरा कम चुभते थे, उस पर पसर गया। ‘अब ?’
यह भी आदत-सी बन गई थी-जब तब, किन्हीं दो स्थितियों के बीच, अपने से सवाल पूछ लेना। जाने कब और कितनी जगह अपने मुँह से यह शब्द सुना था। उसी दिन। उससे एक दिन पहले। हफ्ता भर पहले महीना भर पहले जैसे कि हर नई बार इस शब्द को सामने रख लेने से एक नई तरह से सोचने की शुरुआत हो सकती हो। पर होता इससे कुछ नहीं था-सिवा इसके कि सोच के उलझे हुए धागे में एक गाँठ और पड़ जाती थी। सात दस। अब ? सात पचीस। अब ? सात सैंतालीस। अब ? सात अट्ठावन। अब ? जैसे कि नींद लाने के लिए एक गिनती की जा रही हो। भेड़ों की गिनती की तरह। अब ? अब ? अब ?
खिड़कियों के बाहर सब कुछ अँधेरे में घुल गया था। हर काँच पर काले फौलाद का एक-एक शटर खिंच गया था। यूँ दिन में भी उस सोफे पर बैठने से सिवा पेड़ों की टहनियों और यहाँ-वहाँ उगे घास-पात के कुछ नज़र नहीं आता था। पर शाम को सात के बाद तो कुछ भी सामने नहीं रह जाता था-स्याह काँच और फटी जाली को छोड़कर। पहले एक काँच पर सड़क के लैम्प की रोशनी पड़ा करती थी। उससे वह लैम्प, उससे नीचे का खम्भा और सड़क का उतना-सा हिस्सा रात भर सजीव रहते थे। पर अब कई दिनों से वह लैम्प जलता ही नहीं था। पता नहीं बल्ब फ्यूज हो गया था या लाइन ही कट गई थी। इससे बाहर अँधेरा होने का मतलब होता था बिलकुल अँधेरा। जाकर काँच से आँख सटा लो, तो भी सिवा अँधेरे के कुछ नहीं।
सोफा चेयर पर मुझे काभी असुविधा हो रही थी। रोज होती थी। उसके स्प्रिंग अपेक्षाकृत कम चुभते थे, पर चुभते तो थे ही। वे शिवचन्द्र नरुला लकी बैठन के अनुसार ढले थे। या उससे पहले जो हिंदी मास्टर था, उसकी। पर जिस किसी की बैठन के अनुसार ढले हों, पिछले तीन सालों में वे मेरी बैठन के आदी नहीं हो पाए थे। हम दोनों के बीच एक बेगानापन था, जिसकी शिकायत हम दोनों को रहती थी। अपनी-अपनी शिकायत का गुस्सा भी हम एक-दूसरे पर निकालते रहते थे। वह मुझे स्प्रिंग चुभोकर, मैं उस चुभन को पीसकर। साधारणतया होना यह चाहिए था कि इतने अरसे में मेरी बैठन उन स्प्रिंगों के मुताबिक ढल जाती। पर ऐसा हुआ नहीं था। मेरी बैठन का अपना कसाव स्प्रिंगों के कसाव से कम नहीं था। यह अब और ऐसे नहीं चल सकता’, और अपनी बैठन और स्प्रिंग के बीच हाथ रखे सोचा। ‘जो भी निश्चय करना हो, वह अब मुझे कर ही लेना चाहिए।’’
|
|||||











_s.jpg)